
19-09-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:19-09-20
Date:19-09-20
Reform friction
Centre mustn’t buckle, small farmers matter
TOI Editorials
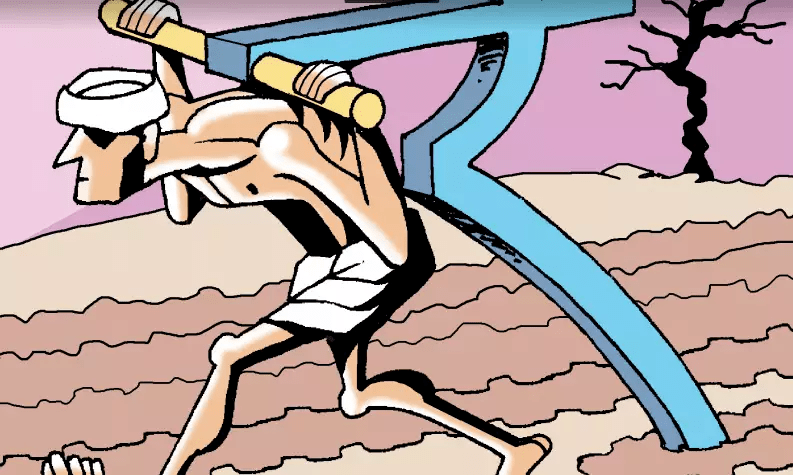
The criticism of federal overreach needs to factor in the big picture. States are unable to usher in such reforms as they are often hostage to big farmer and middlemen lobbies. By striking compromises on GST compensation, Centre could have offset the complaints of states of revenue loss for sales outside APMCs. PM Modi has made a weighty promise to farmers, 86% of whom are small and marginal farmers, to double their incomes by 2022. The status quo, including minimum support prices, isn’t helping enough farmers unlike direct benefit transfers, besides distorting markets and cropping patterns too.
Centre has clarified that it isn’t undermining APMCs or MSPs but merely increasing competition by allowing agribusinesses, food processors, wholesalers, exporters and big retailers to source directly from farmers. Opposition parties are joining the protests for political mileage, but government must improve its messaging on the salience of these reforms. Besides politicisation, the other weakness is the variance between policy and practice. Despite amending the Essential Commodities Act to remove stockholding limits and intemperate regulations on most commonly consumed commodities, Centre has again banned onion exports. Such moves run counter to the professed desire to find new export markets and hinder farmers from securing the benefit of even small increases in wholesale prices.
Welcome reform on the farm front
ET Editorials
The government has shown remarkable conviction in pushing ahead with three Bills designed to change the operating framework of agriculture in India, even in the face of resignation from the council of ministers of the representative of an old-time ally, the Akali Dal. This is commendable. The core of the reform sought to be delivered by the Bill is laudable and necessary.
One Bill frees farmers from the grip of the Agricultural Produce Marketing Committees (APMC) and gives them marketing freedom. Farmers can have that freedom only if their customers — traders, agro-processing companies — have similar freedom to buy and stock farm produce. The Bill amending the Essential Commodities Act frees traders from arbitrary stocking limits and the threat of penalties for hoarding. The third Bill seeks to legitimise and regulate contract farming. All three are interrelated, and, together with the financing plans arranged for post-harvest food-handling infrastructure, promise to give farming in India an incentive to move away from subsistence and towards market orientation. While the government has sought to assuage farmer anxiety by asserting that minimum support prices (MSPs) are not going to disappear, the fact remains that the logic of the changes proposed, and the compulsions of grain production, storage and international trade, point to phasing out of open-ended procurement at MSP. The current ridiculous situation of about one-third of the country’s grain output ending up in government stocks, only there to rot or be pilfered, is unsustainable. Northwest India has to shed over-reliance on grain and diversify production to fruit, flowers, vegetables and other produce, and integrate more stages of value addition into the farmer’s ambit.
The Bill on marketing freedom keeps disputes out of the courts, and depends on the efficacy and fair-mindedness of civil servants for dispute resolution. That might be neither legally tenable nor desirable. Central legislation on intra-state trade is contentious. An effort to find common ground is in order.
Date:19-09-20
Her Majesty’s Parliament
Arghya Sengupta & Lalit Panda, [ Sengupta and Panda are research director and research fellow, public law, respectively, Vidhi Centre for Legal Policy, New Delhi ]
Indians have been asking questions in legislative bodies since British colonial times. Those were times, of course, when legislatures didn’t have the same legitimacy or powers as they now do under the Constitution. Perhaps this is exactly why India’s British rulers first allowed it. What difference does a question make when nothing much turns on it?
Our political class made a conscious decision to continue with this colonial parliamentary tradition after Independence in the form of Question Hour — a one-hour period reserved for members of Parliament (MPs) to ask questions, usually of ministers, regarding the functioning of their ministries. By all accounts, Parliament has been consistently conducting Question Hour in all its sessions except on some occasions, typically during wars and the Emergency.
Despite this hoary tradition, we seem to be back to square one today, although in a modern, democratic, independent 21st-century republic. Over the last decade, Parliament has become less an institution of accountability, and more a forum for political grandstanding. Disruptions have become normalised. A 2016 Vidhi Centre for Legal Policy study (bit.ly/3hHCDav) has shown that both when NDA was in opposition in 2013 and when UPA was in opposition in 2015, close to 60% of parliamentary time was spent on disruptions.
Even during productive hours, the time spent actually asking and answering questions was low. For example, in the 2015 monsoon session of the Rajya Sabha, of the 270 starred questions, only six were answered orally, taking up only 10 minutes of the total 541minutes that the House was productive.
This is by no means unique to Parliament. Many state legislatures have an even more woeful record of sittings and deliberation. In this context, the decision to suspend Question Hour in the ongoing monsoon session of Parliament and in a few state legislatures is unsurprising. After all, much like in colonial India, very little seems to turn on answering questions in legislative bodies any more. But the diminishing productivity of legislatures can scarcely be a justification for the suspension of their functions. The argument that Question Hour is wasted on our political class because they are more interested in disruptions anyway is intuitive, but badly misses the point. We cannot demand that members in the Opposition should behave in a civilised manner by actually removing the things that make civilisation worthwhile: the opportunity for open disagreement, deliberation, concern for those in different circumstances, and accommodation.
Suspended Animation?
In theory, questioning government is the heart and soul of a deliberative democracy. Democracy cannot simply be equated to the hyper-simplified grant of consent that voting represents. If we become fixated merely on voting as a form of communication of our views, we forget the simple reality that our views aren’t fixed and that the increased availability of relevant information can change views and persuade individuals to accommodate their opponents to the maximum extent that their convictions permit. Sharp questions lead to better decisions and more opportunities for bipartisan consensus.
They equally lead to demonstrable accountability, the raison d’ê tre of Parliament. The classic illustration remains the questioning of finance minister T T Krishnamachari in 1957 regarding certain investments made by the government-controlled Life Insurance Corporation (LIC) of India. While Krishnamachari denied any wrongdoing, dogged inquiry by MPs eventually led to the appointment of a commission of inquiry, the unearthing of a financial scam, and the resignation of the minister responsible.
Despite their obvious utility, parliamentary questions — and an hour in Parliament to ask them — are anathema today. Much of this has to do with the fact that most political communication is one-way through social media. Even when there are discussions, they are often in the echo chambers that social media naturally tends to create. In such an atmosphere of facile agreement, questions may seem like an affront. Equally, those speaking truth to power are often complicit in putting themselves above the issues they agitate about.
Discussion, debate and consensus are readily replaced by hectoring, righteousness and lack of self-reflection. Questions, in this context, are an anachronistic annoyance to quick and effective governance.
The coronavirus pandemic is a poor ruse to suspend Question Hour that ought not to fool anyone. Is there more of a chance of the virus spreading if members ask and answer questions, as opposed to speak on Bills and motions? Or, if the time period of each sitting has to be shortened, why should the reduction not be even across the board?
Not Just Figure of Speech
It is clear to anyone who can see that suspending Question Hour, albeit temporarily, in both the Centre and a few states, is the symbol of a deeper malaise incipient over the last two decades — the disdain for legislatures shared by many governments in power.
Legislatures are viewed as fora to pass Bills, not improve them; to make proposals and not reflect upon them; to deliver speeches and not engage with them. Without serious introspection and reinvention, Parliament and state legislatures may soon become like those colonial councils set up with Her Majesty’s blessings: lacking in substance, even where all the forms are followed.
Market failure
New deal for agriculture needs good regulated markets ahead of private competition
EDITORIAL
The ambitious initiative of the Narendra Modi government to bring about far-reaching reform in agriculture has run into severe weather, mainly over fears that the free market philosophy at its core could spell the end of MSPs for produce that has so far been centrally procured by the government. An allied party’s Minister, Harsimrat Kaur Badal (Akali Dal) has resigned in protest, and there is a strong pushback from farmers against three Bills that seek to replace ordinances issued in June, on key aspects of the farm economy — trade in agricultural commodities, price assurance, farm services including contracts, and stock limits for essential commodities. The opposition to the Bills, particularly on trade, flows from the position, articulated by Punjab, that agriculture and markets are State subjects, and there should be no tinkering with the MSP and Agricultural Produce Market Committees (APMC), that form the backbone of existing trading arrangements. Several States have already liberalised agricultural marketing, amending their APMC Acts, and some have allowed regulated private commerce including direct marketing. Yet, provisions in the Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020, providing for unfettered commerce in designated trade areas outside APMC jurisdictions without levy of any fee, and more generally, empowering the Centre to issue orders to States in furtherance of the law’s objectives, have alarmed States. A challenge has been mounted by Rajasthan, declaring central warehouses as procurement centres under its APMC Act, and therefore required to pay a market fee to the State.
Mr. Modi has characterised the arguments as misleading, promising that the MSP system will continue. This is welcome, but the new dispensation cannot bring cheer to small farmers, who form the majority and whose access levels to markets under the APMC system are at the rate of one for an area of 434.48 sq. km on average — well below the recommendation of the National Commission on Farmers (NCF), at one market for 80 sq. km. There is evidence also that mere liberalisation does not lead to private investment in new markets. When Bihar removed the APMC system, markets suffered loss of fee revenue, with no significant private investments in the sector. If the Centre’s intent is to strengthen competition, it should massively fund the expansion of the APMC market system, removing trade cartels, and providing farmers good roads, logistics of scale and real time information. Rather than opt for heavy centralisation, the emphasis should be on empowering farmers through State Farmers Commissions recommended by the NCF, to bring about a speedy government response to issues. Without strong institutional arrangements, laissez-faire policy may harm lakhs of unorganised small farmers, who have been remarkably productive and shored up the economy even during a pandemic.
बिना कानून बनाए डिजिटल जासूस को कैसे रोकेंगे
विराग गुप्ता
कोरोना के बाद अब चीन ने डिजिटल जासूसी से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है. चीनी कंपनी द्वारा सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर बड़े अपराधियों की डिजिटल कुंडली बनाए जाने के बड़े खुलासे से पूरे देश में हडकंप है। इस तरह की डाटा चोरी के पांच पहलू हैं। देश की सुरक्षा में सेंध, लोकतांत्रिक और चुनावी व्यवस्था में हस्तक्षेप, प्राइवेसी में दखलंदाजी, वैश्विक संचार तंत्र पर कब्जा, और बाजार में माल बेचना। ऑपरेशन प्रिज्म के माध्यम से 14 साल पहले अमेरिका ने भारत की सुरक्षा में सेंध लगाई थी। उस मामले का खुलासा करने वाले स्नोडेन को अमेरिका से भागना पड़ा था।
डाटा चोरी करने वाली कंपनियां विश्व में सिरमौर बन गई हैं। उसके बाद कैंब्रिज एनालिटिका-फेसबुक के माध्यम से भारत की चुनावी व्यवस्था में हस्तक्षेप की कोशिश हुई, जिसकी सीबीआई जांच के परिणामों का कोई अता-पता नहीं है। पेगासस-वॉट्सअप मामले में प्राइवेसी में दखलंदाजी के आपराधिक साक्ष्य मिलने के बावजूद सरकार और विपक्ष दोनों मौन ही बने रहे। ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट का नया बाजार तो संचार तंत्र को कब्ज़ा करके ही बना है।
सस्ता डाटा, इंटरनेट और स्मार्टफोन के विस्तार से भारत डाटा का वैश्विक महासागर बन गया है. लोगों का नाम, फोटो, ईमेल, मैसेज, वीडियो, मोबाइल नंबर, और लोकेशन का डाटा डिजिटल मंडी में कौड़ियों के भाव नीलाम हो रहा है। डाटा माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विदेशी कंपनियों ने भारत के बाजार और सामरिक तंत्र में पूरा कब्ज़ा कर लिया है। चीनी कंपनी ने रटंतु जवाब में कहा है कि सार्वजनिक डाटा इकट्ठा करने के व्यापार में कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। सार्वजनिक डाटा के इस्तेमाल के खिलाफ स्पष्ट कानून भले ही ना हो, लेकिन सरकारी, सामरिक और जनता के निजी संवेदनशील डाटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ भारतीय कानून के अनुसार अपराध है। पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेटस एक्ट जैसे कानून की वजह से सरकारी कार्यों में विदेशी ईमेल और नेटवर्क के इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध है। सोशल मीडिया कंपनियां भारत के ग्राहकों का डाटा विदेश में रखती हैं, इसलिए सोशल मीडिया के सरकारी इस्तेमाल पर भी अनेक प्रतिबंध हैं। सरकारी मोबाइल और कंप्यूटर नेटवर्क से इंटरनेट और सोशल मीडिया को कनेक्ट करने पर भी अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं। लेकिन इन नियमों का पालन नहीं होने से सरकारी और सामरिक सूचनाएं चीन और अन्य विदेशी शक्तियों तक बेरोकटोक पहुंच रही हैं, जो राष्ट्रीय चिंता का विषय है। चीनी कंपनी की तर्ज़ पर डाटा प्रोफाइलिंग का रिवाज़ यदि बढ़ा तो नेता, अफसर और जजों को ब्लैकमेल करने का नया सिलसिला, राष्ट्रीय संकट का सबब बन सकता है।
चीनी एप्स पर प्रतिबन्ध को भारत में अभी तक पूरी सफलता से लागू नहीं किया जा सका है। भारत में इस्तेमाल हो रहे तीन चौथाई फोन चीनी हैं, जो डिजिटल जासूसी का सबसे बड़ा माध्यम हैं। चीनी कंपनी ने पूरे विश्व में लगभग 25 लाख लोगों की डाटा प्रोफाइलिंग की है, जिसमें भारत के 10 हजार लोग और संस्थाएं शामिल हैं। लेकिन मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया कंपनियों ने भारत के 130 करोड़ लोगों की डाटा प्रोफाइलिंग करके पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। चीनी कंपनी ने सूचनाओं को हासिल करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टिकटॉक, गूगल, लिंक्डइन जैसे प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया। कैम्ब्रिज एनालिटिका की तर्ज़ पर फेसबुक ने चीनी कंपनी को दी गई इजाजत को रद्द कर दिया है। सवाल यह है कि फेसबुक जैसी कंपनियां ग्राहकों की स्पष्ट सहमति के बगैर दूसरे एप्स को डाटा माइनिंग की गैरकानूनी इजाजत क्यों देती हैं? सवाल यह है कि जब डाटा और ओटीटी दोनों के बारे में कानून नहीं बनाए जा रहे हैं तो फिर डिजिटल जासूसी को भविष्य में कैसे रोका जा सकेगा? लद्दाख में हमारी सेना ने चीन को पीछे धकेल दिया। लेकिन चीनी सेना द्वारा समर्थित हाइब्रिड वार फेयर यानी डिजिटल युद्ध से मुकाबले में भारत बहुत पीछे है। चीन का यह निगरानी तंत्र डिजिटल जासूसी का एक छोटा ट्रेलर है। इस मामले से सबक लेकर सरकार और संसद द्वारा समुचित कार्रवाई हुई तभी आगे चलकर ऐसे मामलों को रोकने में कामयाबी मिल सकेगी।
ब्रेक्सिट का जनमत संग्रह और 2016 के अमेरिकी चुनावों में सोशल मीडिया कंपनियों के माध्यम से रूस ने व्यापक हस्तक्षेप किया। भारत में अनेक पार्टियों की सोशल मीडिया कंपनियों के साथ सांठगांठ के सबूत उजागर हो रहे हैं। इस मामले के खुलासे के बाद बिहार और बंगाल के चुनावों में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप की आशंका बढ़ गई है।
वोटर लिस्ट को सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म्स और लोकेशन के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो मतदाताओं के रुझान को बदला जा सकता है। चीन और अमेरिकी सरकारों द्वारा समर्थित विदेशी डिजिटल कंपनियों के माध्यम से नेताओं ने वोटरों को कब्जाने का मंत्र हासिल कर लिया तो फिर आने वाले समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था बेमानी हो जाएगी।
संदेह के बीज बोन के नाम
संपादकीय
बिहार की विकास योजनाओं के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा से पारित कृषि विधेयकों का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को जिस तरह निशाने पर लिया, उससे यह साफ है कि उन्हें इसका आभास हो रहा है कि यह मामला एक राजनीतिक मसला बनता जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस को खास तौर पर निशाने पर लिया तो इसके पीछे पर्याप्त कारण हैं। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनावों के समय अपने घोषणा पत्र में यह दर्ज किया था कि यदि वह सत्ता में आई तो कृषि उत्पाद बाजार समिति कानून यानी एपीएमसी एक्ट को खत्म करने के साथ कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री को प्रतिबंधों से मुक्त करेगी। अब जब यही काम किया जा रहा है तो कांग्रेस विरोध का झंडा बुलंद कर रही है। यह सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। कांग्रेस का यह रवैया नया नहीं है। उसने यही काम नागरिकता संशोधन कानून के मामले में भी किया था। एक समय इस कानून में जैसे संशोधन की मांग उसके नेता संसद में कर रहे थे, वैसे संशोधन हो जाने पर उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया था। जैसे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोगों को भड़काने में कांग्रेस सबसे आगे रही, उसी तरह कृषि विधेयकों के खिलाफ भी वह किसानों को उकसाने में बढ़-चढ़कर सक्रिय है। यह पंजाब में कांग्रेस की ओर से कृषि विधेयकों के उग्र विरोध को हवा देने का ही परिणाम रहा कि शिरोमणि अकाली दल भी उससे होड़ लेने के लिए आगे आ गया।
यह हास्यास्पद है कि शिरोमणि अकाली दल के जिन नेताओं ने तीन माह पहले कृषि सुधारों से जुड़े अध्यादेश जारी होने पर उनका स्वागत किया था, वे अब यह कह रहे हैं कि इस मामले में उनसे सलाह नहीं ली गई। कृषि सुधारों का विरोध कर रहे दल और संगठन भले ही किसानों के हितों की दुहाई दें, लेकिन सच यही है कि वे अनाज मंडियों में वर्चस्व रखने वाले आढ़तियों और बिचौलियों के हितों को साधने के लिए किसानों के मन में संदेह के बीज बो रहे हैं। इस ओर संकेत करते हुए प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि कुछ राजनीतिक दल किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के किसान बिचौलियों और उनकी ढाल बने दलों के बहकावे में इसलिए आ गए हैं, क्योंकि एक तो वे नई व्यवस्था से अच्छी तरह परिचित नहीं और दूसरे, उन्हें यह भरोसा नहीं हो पा रहा है कि उससे उनकी मुश्किलें कम होंगी। बेहतर हो कि सरकार किसानों की आशंकाएं दूर करने के लिए और अधिक सक्रिय हो।
![]() Date:19-09-20
Date:19-09-20
भारत-चीन के बीच अंतर
टी. एन. नाइनन

एशिया में दो बड़ी ताकतों के उदय की कहानी तीन दशक पुरानी है और इसकी मियाद बीत चुकी है। चीन हर मोर्चे पर भारत को पीछे छोड़ चुका है और अब वह समूचे एशिया पर दबदबा चाहता है। शक्ति का असंतुलन हर मोर्चे पर स्पष्ट है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। चीन अब बीते दौर की इकलौती महाशक्ति को चुनौती दे रहा है जबकि भारत को अपने ही भूभाग को बचाने की कवायद करनी पड़ रही है। यह सही है कि दोनों देश समांतर कालखंड में प्रगति करते रहे हैं लेकिन दोनों की सफलता के परिमाण को देखें तो यह निरर्थक है।
आज चीन की स्थिति वैसी नहीं है जैसी सन 2010 में थी। उस वक्त मनमोहन सिंह और चीन के प्रधानमंत्री वेन च्यापाओ ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा था, ‘दुनिया में भारत और चीन दोनों के विकास के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। निश्चित रूप से दोनों देशों के सहयोग के लिए भी ढेर सारे क्षेत्र मौजूद हैं।’ इसके बाद भारत का प्रदर्शन जहां कमजोर पड़ता गया, वहीं चीन ने ताकत और प्रभाव दोनों बढ़ाया। इससे शक्ति संतुलन और अधिक डगमगा गया। चीन दुनिया का प्रमुख विनिर्माता है। वह सबसे बड़ा विनिर्मित वस्तु निर्यातक है और उसने अद्यतन तकनीक के साथ बढ़त बनाई है जिनमें से कई का सैन्य इस्तेमाल संभव है। हमारा सामना एकदम अलग किस्म के चीन से है। ऐसे में समानता का दिखावा दरअसल मुसीबत को न्योता है।
इस संदर्भ में सेवानिवृत्त राजनयिक राजीव डोगरा की नई किताब ‘इंडियाज वल्र्ड: हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स शेप्ड फॉरेन पॉलिसी’ पढऩा जानकारीपरक होगा। उसमें दिए संदर्भ के मुताबिक सन 1962 की जंग के समय चीन के राष्ट्राध्यक्ष रहे लिउ शाओछी ने श्रीलंकाई राजनेता फेलिक्स भंडारनायके से कहा था कि सन 1962 की लड़ाई भारत का अहंकार और श्रेष्ठता का भ्रम तोडऩे के लिए हुई थी। अब इस बात के साथ गृहमंत्री अमित शाह के गत वर्ष लोकसभा में दिए भाषण को याद कीजिए जहां उन्होंने कहा था, ‘जब भी मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन शामिल होते हैं और हम इसके लिए जान भी दे देंगे।’ जमीनी हकीकत से वाकिफ कोई भी व्यक्ति इस बात को खारिज कर देता। चीन ने यही संदेश लिया होगा कि भारत पुन: ‘अहंकारी’ हो रहा है।
पॉल केनेडी ने अपनी किताब ‘द राइज ऐंड फाल ऑफ द ग्रेट पावर्स’ में आर्थिक परिवर्तन के बीच सैन्य विवादों तथा अर्थशास्त्र और सामरिक नीति के बीच के संंबंधों की बात की है। उनके मुताबिक किसी देश का उदय या पराभव युद्ध के समय नहीं बल्कि शांतिकाल में होता है और यह अन्य ताकतों के सापेक्षिक होता है, न कि विशिष्ट। जयशंकर की टिप्पणी को केनेडी की दलील पर कस कर देखें तो भारत ने चीन के साथ अपनी चर्चा में इस बात की अनदेखी कर दी कि यहां दोनों देशों के साथ-साथ विकास जैसी परिस्थितियां हैं भी या नहीं।
अच्छी बात यह है कि बातचीत के दौरान भारत खाली नहीं बैठा। उसने अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ाकर चीन के साथ शक्ति असंतुलन दूर करने का प्रयास किया। उसने लद्दाख तक पहुंच की खातिर सीमा पर हर मौसम में चलने वाली सड़क बनाने हेतु सुरंग खोदीं, पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाए और विवादित सीमा तक सामान पहुंचाने के रास्ते तैयार कर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया।
दुख की बात है कि करगिल में भी और अभी भी सेना जमीन गंवाने के पहले नहीं जागी। यकीनन सेना 1962 जैसे हालात में नहीं है लेकिन उसका ध्यान इस बात पर है कि और जमीन न गंवाई जाए। बाकी बातें कूटनीति के हवाले हैं।
सीमित बजट से मजबूत सेना नहीं बन सकती। इसके लिए विनिर्माण क्षमता और उन्नत तकनीक भी चाहिए। मानव विकास सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत काफी पीछे है। ऐसे में यह लक्ष्य कठिन हो जाता है। सीमा का गतिरोध और उससे जुड़ी अनिश्चितता में एक चेतावनी निहित है कि हम वास्तविक शक्ति बनने की दिशा में काम करें।
सुधारों से बेचेन क्यों हैं किसान
कृष्ण प्रताप सिंह
2014 में सब कुछ बदल डालने और सारी दुर्दशाएं खत्म कर अच्छे दिन लाने का वायदा करती हुई नरेंद्र मोदी सरकार आई तो किसानों की उम्मीदें भी कुछ कम हरी नहीं हुई थीं। उनका मानना था कि उन्हें ‘अच्छे दिनों’ में बड़ा हिस्सा नहीं भी मिला तो भूमंडलीकरण की अनर्थकारी अर्थनीति द्वारा बरबस थोप दिए गए अन्यायों से तो निजात मिल ही जाएगी। उन्हें क्या मालूम था कि जल्दी ही यह सरकार भी पूर्ववर्तियों की तरह दिखावे की हमदर्दी की राह पकड़ लेगी-खाने के दांत भूमंडलीकरण की पैरोकार बड़ी पूंजी को दे देगी और बाकियों को दिखाने के दांतों का सब्जबाग छोड़ कुछ नहीं पाने देगी। 2019 में दोबारा चुनकर आएगी तो भी सबका विश्वास जीतने की ईमानदार कोशिशों के बजाय फांसे रखने की शातिर चालाकियों से काम लेगी।
सरकार ने 2017 के अप्रैल महीने में ही संकेत दे दिए थे कि कुछ भावनात्मक फंसंतों को छोड़कर उसके पास किसानों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब, जब महीने भर से राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रहे तमिलनाडु के किसानों का धैर्य इस कदर टूट गया था कि उन्होंने साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई शर्म नहीं महसूस की थी। तब भी नहीं, जब किसानों ने भयंकर सूखे व कर्ज के बोझ से जिंदगी हार जाने वाले अपने परिजनों की खोपड़ियां हाथों में लेकर, सिर मुंडवाकर और साड़ियां पहनकर प्रदर्शन किया और स्वमूत्रपान की कोशिश भी की। बाद में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व दूसरे कई राज्यों में अनसुनी से आजिज किसान अपनी उपजों के वाजिब दाम और कर्जमाफी वगैरह की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे तो भी सरकार उनसे अपनों की तरह नहीं ही पेश आई।
फिर भी किसानो ने अपने धैर्य से बचाये रखा,लेकिन अब वह कृषि सुधार के नाम पर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमो से पूरी तरह टूट जाने की ओर बढ़ता लगता हैं इन सुधारों के तहत अब अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू वगैरह न ‘आवश्यक वस्तुएं’ हैं और न ही इनकी जमाखोरी या कालाबाजारी कानूनन अपराध है। सरकार बता रही है कि किसानों की इन उपजों को उनके भले के लिए ही ‘मुक्त’ बाजार के हवाले किया गया है, लेकिन यह नहीं बता रही कि अब इनकी खरीद-बिक्री में बड़ी रिटेल कंपनियां प्रमुख खिलाड़ी होंगी, जो किसानों से अपनी शर्तों पर इन्हें खरीदेंगी और बेचेंगी।
पता नहीं इस सरकार को ‘एक देश, एक….’ की तुकबंदी से कितना लगाव है कि कभी वह ‘एक देश, एक चुनाव’ की बात करती है, कभी ‘एक देश, एक राशनकार्ड’ की, कभी ‘एक देश, एक भाषा’ की और कभी ‘एक देश, एक बाजार’ की। अगर यह सारे देश को एक डंडे से हांकने की उसकी किसी परियोजना का हिस्सा है तो उसे समझना चाहिए कि विविधताओं से भरा यह देश इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरकार से पूछा ही जाना चाहिए कि वह अपनी तुकबंदी को ‘एक देश, एक आय’ जैसी किसी योजना तक क्यों नहीं पहुंचाती? बहरहाल, किसान इतने भर से ही खफा नहीं हैं। इसलिए भी खफा हैं कि इन कृषि सुधारों के तहत सरकार उन्हें मंडियों के बाहर भी उपज बेचने की जो ‘सहूलियत’ दे रही है, वह भी ‘एक देश, एक कृषि बाजार’ की तरह उनके लिए कोढ़ में खाज ही सिद्ध होगी। तिस पर अनुबंध आधारित खेती को कानूनी वैधता उन्हें अपने ही खेतों में मजदूर बनाकर छोड़ेगी।
तथाकथित कृषि सुधारों के तहत बिचौलियों और व्यापारियों की भूमिका बढ़नी ही है कृषि उपजों की मंडियों से बाहर खरीद-बिक्री का मतलब किसानों को बड़े गल्ला व्यापारियों के रहमोकरम पर छोड़ देने के अलावा कुछ नहीं है। दरअअल, ये व्यापारी ही ‘एक देश, एक कृषि बाजार’ के वास्तविक लाभार्थी होंगे, जो किसानों से औने-पौने दाम में उनकी जिंसें खरीदकर अपनी सुविधा व लाभ के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में बेचेंगे। ऐसे में साफ है कि किसानों का नए बंटाधार के अंदेशों से हलकान होना व सड़कों पर उतरना अकारण नहीं है। बेहतर होगा कि सरकार इन सुधारों पर अड़ी रहकर निवेशकों व पूंजीपतियों के हितों का पोषण करती रहने के बजाय किसानों को आश्वस्तिकारी संदेश देने के लिए अपने कदम पीछे खींच ले। इस कठिन समय में बेरोजगारों व युवाओं के साथ किसानों को भी उद्वेलित करना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होगा। क्योंकि वे राजद्वार ऊंचे करते रहने के लिए हमेशा अपनी झोंपड़ियां झुकाते नहीं रह सकते।
कृषि में बदलाव
संपादकीय
कृषि संबंधी तीन विधेयकों के लोकसभा से पारित होते ही देश के अनेक हिस्सों में राजनीति का गरमाना जितना स्वाभाविक है, उतना ही चिंताजनक भी है। किसानों के प्रदर्शन से लाभ कम और नुकसान ज्यादा होता है, अत: नुकसान से बचने की कोशिश हर स्तर पर करते हुए उनका विश्वास जीतना चाहिए। केंद्र सरकार के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने न सिर्फ इस्तीफा दे दिया, बल्कि उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। सरकार ने अपनी ओर से साफ संकेत दे दिया है कि वह इस मामले में पीछे नहीं हटेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि संबंधी विधेयकों की पैरोकारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जो किसानों से कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे किसानों को बचाने के लिए इन विधेयकों को लाना बहुत जरूरी था। उन्होंने यह भी कहा कि ये तीनों विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर आए हैं। प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप ही किसानों को विश्वास में लेने की जरूरत है।
सरकार को संवाद के रास्ते पर चलते हुए सभी विरोधियों को आश्वस्त करना चाहिए था, पर जिस तरह से पुरानी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल को निराश किया गया है, वह अनेक लोगों को चौंकाएगा। अकाली दल अब सरकार से समर्थन वापस लेने की भी घोषणा कर सकता है, हालांकि इससे केंद्र सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरह से विगत के अनेक बदलावों के प्रति केंद्र सरकार दृढ़ रही है, वैसी ही दृढ़ता इस मामले में दिख रही है। दरअसल, पंजाब और हरियाणा की राजनीति किसानों द्वारा संचालित रही है। पार्टियों और नेताओं में खुद को किसान सिद्ध करने की होड़ रहती है, ऐसे राज्य में शिरोमणि अकाली दल के केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर जाने का सीधा अर्थ है कि यह दल किसानों के विरोध को झेलने की स्थिति में नहीं है। लोकसभा में विधेयक के पारित होने से ठीक पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की बजाय काफी पहले ही विरोध स्वरूप हट जाना चाहिए था। ऐन मौके पर इस्तीफा देने के कारण ही प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि किसानों से धान-गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी।
प्रधानमंत्री के इस आश्वासन से किसानों को राहत का एहसास जरूर हुआ होगा। पूरी दुनिया के कृषि बाजार में जो व्यवस्था है, उसे भारत में कमोबेश लागू करना पुरानी मांग है। लेकिन कोई भी बदलाव करते हुए किसानों के हित के साथ-साथ राज्य सरकारों को मंडी से मिलने वाले राजस्व को भी बहाल रखना चाहिए। जो नेता खुद को किसानों का पक्षधर बताते हैं, उन्हें आगे आकर किसानों के लाभ को सुनिश्चित करना चाहिए। कृषि क्षेत्र में खुला बाजार और कंपनियां हमारे देश में नई बात नहीं है, इस खुले बाजार में भी किसानों के हितों की रक्षा करना सरकारों की जिम्मेदारी है। देश में किसानों की बदहाली से सभी वाकिफ हैं, इसलिए उनकी हरेक चिंता का निवारण करना सरकारों का प्राथमिक दायित्व है। यह भी ध्यान रहे, किसानों का शोषण करने वाले लोग विदेश से नहीं आते, यहीं हमारे बीच से खड़े होते हैं। कृषि और कृषकों के दुश्मन दलालों और कंपनियों को स्थानीय स्तर पर ही संगठन की शक्ति से नियंत्रित करना होगा।
Date:19-09-20
किसानों के देश की अपनी चिंताएं
मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की हमारी व्यवस्था दुनिया के लिए मॉडल बन सकती है,सरकर इस मॉडल को भी नहीं छोड़ना नई चाहती।
देविंदर शर्मा
अमेरिका के एक किसान ने ट्वीट किया कि उसने 2018 में मक्का जिस कीमत पर बेचा, मक्के की उससे ज्यादा कीमत उसके पिता को 1972 में मिली थी। यह एक ऐसे देश की दशा है, जहां छह-सात दशक से खुला बाजार है। अभी हाल ही में अमेरिकी कृषि विभाग के एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि अमेरिकी किसानों की आय तेज गिरावट की ओर है। इससे पता चलता है कि जो बाजार सुधार अमेरिका ने कृषि क्षेत्र में सात दशक पहले किया था, वह नाकाम साबित हो चुका है। इस साल अमेरिका के किसानों पर 425 अरब डॉलर का कर्ज हो गया है। वहां ग्रामीण इलाकों में आत्महत्या की दर शहरों से 45 प्रतिशत ज्यादा है। यह वह देश है, जहां खुला बाजार है, जहां बड़ी कंपनियों के लिए कोई भंडार सीमा नहीं है। अनुबंध खेती और वायदा बाजार भी है। वहां एक देश एक बाजार ही नहीं, एक दुनिया एक बाजार है। वहां के किसान दुनिया में कहीं भी निर्यात कर सकते हैं, इसके बावजूद वहां कृषि पर संकट गंभीर है।
अगर हम यूरोप में देखें, तो फ्रांस में एक साल में 500 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अमेरिका में वर्ष 1970 से लेकर अभी तक 93 प्रतिशत डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं। इंग्लैंड में तीन साल में 3,000 डेयरी फार्म बंद हुए हैं। अमेरिका, यूरोप और कनाडा में सिर्फ कृषि नहीं, बल्कि कृषि निर्यात भी सब्सिडी पर टिका है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, हर साल 246 अरब डॉलर की सब्सिडी अमीर देश अपने किसानों को देते हैं। बाजार अगर वहां कृषि की मदद करने की स्थिति में होता, तो इतनी सब्सिडी की जरूरत क्यों पड़ती? हमें सोचना चाहिए कि खुले बाजार का यह पश्चिमी मॉडल हमारे लिए कितना कारगर रहेगा?
गौर करने की बात है, वर्ष 2006 में बिहार में अनाज मंडियों वाले एपीएमसी एक्ट को हटा दिया गया। कहा गया कि इससे निजी निवेश बढ़ेगा, निजी मंडियां होंगी, किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। आज बिहार में किसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे जिस अनाज के लिए 1,300 रुपये प्रति क्विंटल मिलते हैं, उसी अनाज की कीमत पंजाब की मंडी में 1,925 रुपये है। पंजाब और हरियाणा में मंडियों और ग्रामीण सड़कों का मजबूत नेटवर्क है। इसी वजह से पंजाब और हरियाणा की देश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका है।
अब जब वैध रूप से मंडी के बाहर भी अनाज बिकेगा, तो एक देश दो बाजार हो जाएगा। मंडी में जो खरीद होगी, उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन मंडी के बाहर होने वाली खरीद पर नहीं लगेगा। इस वजह से मंडियां धीरे-धीरे खाली होती जाएंगी। सरकार का कहना है हमने एपीएमसी को नहीं छुआ है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी रहेगा, पर किसानों को शंका है कि जब एपीएमसी का महत्व कम होगा, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का महत्व भी खत्म हो जाएगा।
शांता कुमार समिति कहती है कि देश में सिर्फ छह प्रतिशत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है और 94 प्रतिशत किसान खुले बाजार पर निर्भर हैं। साफ है, अगर खुला बाजार अच्छा होता, तो किसानों की समस्या इतनी क्यों बढ़ती? अगर खुले बाजार में किसानों को उचित मूल्य मिल रहा होता, तो वे भला क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते?
ओईसीडी की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 व 2016 के बीच भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हें उचित दाम नहीं मिला। आर्थिक सर्वेक्षण 2016 कहता है, किसान परिवार की औसत आय देश में सालाना 20,000 रुपये है। बड़ा सवाल है कि इतने कम पैसे पर किसान परिवार जीवित कैसे रहता होगा?
अब सरकार पांच साल तक की अनुबंध खेती को भी मंजूरी दे रही है। उपज की कीमत पहले तय हो जाएगी। कोई समस्या होगी, तो पहले एसडीएम के पास जाना पड़ेगा। इतिहास रहा है, कंपनी की ही ज्यादा सुनी जाएगी। एक और बड़ी बात हुई है कि कुछ अनाजों से भंडारण की सीमा हटने से एक तरह से जमाखोरी के रास्ते खुल जाएंगे। किसानों को क्या फायदा होगा? जो नुकसान होगा, उपभोक्ता भुगतेंगे। आज प्याज की जो कीमत बढ़ रही है, उसमें जमाखोरी की भी बड़ी भूमिका है। अमेरिका में वालमार्ट जैसी बड़ी कंपनियां हैं, उनके भंडारण की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वहां तो किसान को फायदा हुआ नहीं, वह तो सब्सिडी पर बचा है। अमेरिका में किसानों को मिल रही औसत सब्सिडी 7,000 डॉलर प्रतिवर्ष है, जबकि भारत में करीब 200 डॉलर। खुले बाजार के बावजूद वहां सब्सिडी की जरूरत क्यों है?
क्या हमें खुली मंडी, अनुबंध खेती व भंडारण संबंधी प्रावधान अमेरिका और यूरोप से लेने चाहिए थे? हमारे प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, आज भारत के पास मौका है, सबका साथ सबका विकास साकार करने का। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत बनाने को प्रयासरत हैं और इन दोनों मंजिलों की राह गांव से होकर गुजरती है। गांवों-किसानों के हित में हमारा अच्छा मॉडल है एपीएमसी मंडियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य का, जो हमने कहीं से उधार नहीं लिया। अभी पूरे देश में 7,000 मंडियां हैं, हमें चाहिए 42,000 मंडियां। नए प्रावधानों के बाद सब बोल रहे हैं कि किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। अच्छा दाम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा ही होना चाहिए, तो फिर समर्थन मूल्य को पूरे देश में वैध क्यों न कर दिया जाए? किसान की आजादी तो तब होगी, जब उसे विश्वास होगा कि मैं कहीं भी अनाज बेचूं, मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलेगा ही। हमारा मॉडल दुनिया के लिए मॉडल बन सकता है। यही किसानों को सुनिश्चित आय दे सकता है। अच्छा है, सरकार इस मॉडल को नहीं छोड़ना चाहती।
देश में करीब 50 प्रतिशत आबादी और 60 करोड़ लोग खेती से जुड़े हैं, उनके हाथों में ज्यादा दाम आएगा, तो अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। अभी हम 23 फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं, यदि हम देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था कर दें, तो 80 प्रतिशत फसलों का सही मूल्य मिलने लगेगा। लेकिन मंडी और समर्थन मूल्य के बावजूद 60 प्रतिशत किसान ऐसे रह जाएंगे, जिनके पास कुछ बेचने को नहीं होगा। उनके लिए किसान आय और कल्याण आयोग बनाना चाहिए, आयोग तय करे कि हर महीने सरकारी कर्मचारी का जो न्यूनतम वेतन है, उसके बराबर किसानों की आय कैसे सुनिश्चित हो। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें देर-सबेर यह करना ही पडे़गा।
