
15-04-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 15-04-25
Unnecessary change
Amending the RTI Act through the Data Protection Bill is unwarranted
Editorial

That the Right to Information Act and the use of RTIs have enhanced the accountability of those in governance in India goes without saying. In the last few years there have been attempts to dilute the provisions of the Act, a landmark one that was passed 20 years ago. Clearly, some in governance and administration have treated the Act and its provisions on transpa rency and disclosure to be encumbrances. A sig- nificant threat has now emerged in the amend- ment to Section 8(1)(1) of the Act, which has been introduced in Section 44(3) of the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023. The Act itself is an outcome of K.S. Puttaswamy (2017), a judg ment that upheld the right of privacy as a funda- mental right under Article 21 of the Constitution. Section 8(1)(j) of the RTI Act allows government bodies to withhold “information which relates to public information” provided its disclosure is not related to public interest or results in an unneces sary invasion of privacy. While doing so, it provides the safeguard that if the Public Information Officer or an appellate authority finds public in- terest in disclosing such information, it could still be available. This safeguard is important. Some information related to public servants, such as college degrees or caste certificates, might be private, but as a recent and controversial case of a bureaucrat using a fake caste certificate showed, such information could be released in public in- terest. Section 44(3) of the DPDP act amends Sec- tion 8(1)() by allowing government bodies to simply withhold “personal information” without the safeguard provisions on public interest or oth- er such exceptions.
In a letter to Congress leader Jairam Ramesh, Union Minister of Information and Broadcasting, Ashwini Vaishnaw defended the amendment, say- ing that Section 44(3) was aimed at preventing the RTI Act’s “misuse” and was to harmonise the requirement of right to privacy and the right to information. He also said that information such as salaries of public officials would still remain accessible through Section 3 of the DPDP Act. But by amending the RTI Act itself – an outcome that was never the intention of K.S. Puttaswamy – and by defining “personal information” vaguely in Section 44(3) of the DPDP Act, authorities could deny RTI requests of previously public data by classifying them as “personal” – and lessen public scrutiny. The RTI Act already harmonises concerns related to the right to information and privacy by subjecting them to the question of public interest. Therefore, the amendment using the DPDP Act is unnecessary and unwarranted. The government must take the concerns of civil society and transparency activists and remove the provision amending the RTI Act, in the DPDP Act.
Date: 15-04-25
चीन से हटने वाली कंपनियों के लिए हम अच्छा विकल्प
संपादकीय
बड़े देशों को वैश्विक नीतियां बनाने के पहले हर पहलू को देखना होता है क्योंकि उनके बार-बार बदलने से साख गिरती है। चीन के हालिया व्हाइट पेपर ने बताया ट्रम्प का ट्रेड घाटे का दावा मात्र ‘ट्रेड-इन- गुड्स’ (यानी वस्तु निर्यात) के आंकड़े के आधार पर है। इसका कारण सस्ता श्रम और खनिजों की उपलब्धता है। चीन ने यह भी बताया कि स्वयं अमेरिकी कंपनियों ने चीन में सामान बना कर और उन्हें एक साल में वहीं बेचकर 490 अरब डॉलर कमाए, जिसका लेखा-जोखा ट्रम्प के गणित में नहीं है। भारत के लिए सुखद बात यह है कि उसका सेवा निर्यात पहली बार वस्तु निर्यात के बराबर पहुंच गया है। अब उसके पास विकल्प है अमेरिका, ईयू और ब्रिटेन (तीन प्रमुख ट्रेडिंग ब्लॉक्स जिनसे भारत अपने वस्तुओं के कुल निर्यात का 38.1% करता है) से अलग-अलग द्विपक्षीय ट्रेड समझौता (बीटीए) अगले 90 दिनों में पूरा करना | भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम आयातक है और अमेरिका से खरीद बढ़ाकर वह ट्रेड घाटे को उस देश के हित में कम कर सकता है। दुनिया के अन्य देश अपना माल अपेक्षाकृत सस्ता बेचकर डॉलर हासिल करते हैं यानी डॉलर का मूल्य बढ़ जाता है और ज्यादा डॉलर छापने से भी महंगाई नहीं बढ़ती । चीन से हटने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत अच्छा विकल्प बन रहा है ।
Date: 15-04-25
क्या ‘चीप – लेबर’ का दोहन ही तकनीकी सफलता है?
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
हाल ही में एक स्टार्टअप सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल की टिप्पणी ने बड़ी बहस छेड़ दी। उन्होंने भारतीय स्टार्टअप के उदय की प्रशंसा की थी, लेकिन साथ ही डीप-टेक और अत्याधुनिक इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया था। उन्होंने कहा, हम फूड डिलीवरी ऐप्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और बेरोजगार युवाओं को चीप लेबर में बदल दे रहे हैं, ताकि अमीर लोग अपने घर से बाहर जाए बिना अपना फूड पा सकें। उनकी बात में दम है। भारत में विशेष प्रकार की टेक कंपनियों का उदय हुआ है, जिन्हें मैं पीएसआर (पुअर सर्विंग रिच) कंपनियां कहता हूं। इनका बिजनेस मॉडल दो प्रमुख स्तंभों पर टिका है : एक बड़ी और समृद्ध आबादी (यानी अमीर) जिसके पास खर्च करने योग्य पैसा और सुविधा के लिए बढ़ती भूख है। और दो, बहुत बड़ी और अपेक्षाकृत अकुशल आबादी (गरीब), जो इस मांग को पूरा करने के लिए कम वेतन पर काम करने को तैयार है। भारत में इन दोनों ही वर्गों के लोगों की कमी नहीं है।
गोल्डमैन सैक्स की एक रिसर्च के अनुसार, लगभग 6 करोड़ भारतीय सालाना 10,000 डॉलर (8.6 लाख रुपए) से अधिक कमाते हैं। ये ही लोग ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी और अन्य सुविधा-केंद्रित सेवाओं के मूल उपभोक्ता हैं। अनुमान है कि यह संख्या 2027 तक बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। अब, चीप लेबर की आपूर्ति पर विचार करें। भारत में असमानता की स्थिति नामक रिपोर्ट में पाया गया है कि प्रति माह 25,000रु. से अधिक कमाने वाले लोग वेतन पाने वाले शीर्ष 10% लोगों में आते हैं। इसलिए, 15,000-20,000 रु. का मासिक वेतन अभी भी आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आकर्षक है। 1.4 अरब की आबादी में करोड़ों लोग इन वेतनों पर काम करने के लिए तैयार हैं।
यदि हम मान लें कि महीने में 25 कार्य दिवस होते हैं तो 20,000 रु. प्रतिमाह के हिसाब से 800 रु. प्रतिदिन का वेतन हुआ। 10 घंटे के कार्य दिवस के लिए 80 रु. प्रतिघंटा । यह 1 डॉलर से भी कम है। सालाना 10,000 डॉलर से ज्यादा कमाने वाला ग्राहक आसानी से ऐसे 50-100 ऑर्डर दे सकता है। इसमें सभी को लाभ है। डिलीवरी करने वाला कर्मचारी औसत से ऊपर का वेतन कमाता है। अमीर लोग मिनटों में ही अपने दरवाजे पर डिलीवर किए गए फूड का मजा लेते हैं। टेक फाउंडर्स को सफलता मिलती है और उनमें से कई तो अरबपति या राष्ट्रीय प्रतीक भी बन जाते हैं।
वैल्यूएशन बढ़ने से शेयरधारक खुश होते हैं। और औसत भारतीय अपने एनआरआई रिश्तेदारों के सामने देश की तकनीकी क्षमता का बखान करता है कि हम साबुन ऑर्डर करते हैं और वह 10 मिनट में आ जाता है। विकसित देश ऐसा कर सकते हैं?
लेकिन यहां पर हम यह अनदेखा कर देते हैं कि यह तभी संभव हो सकता है, जब तक कि एक बड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग किसी भी नौकरी के लिए बेताब न हो। ये वे लोग हैं, जो गांवों से पलायन करके शहर आ रहे हैं, क्योंकि खेती अब लाभदायक नहीं रह गई है। वे शहरों में आते हैं, क्योंकि यहीं ज्यादातर अमीर लोग रहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहीं पर पीएसआर नौकरियां उपलब्ध हैं। अमीर लोग पहले भी खाना पकाने, सफाई करने और गाड़ी चलाने के लिए सेवकों को काम पर रखते थे। लेकिन आज तकनीक ने माइक्रो-पीएसआर के अवसर रचे हैं। आप एक आलीशान अपार्टमेंट में किसी अमीर आदमी के लिए भले काम नहीं कर सकते हों, लेकिन आप उसे एक सैंडविच जरूर डिलीवर कर सकते हैं- और यह आपकी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त होगा।
लेकिन क्या यह वास्तव में अत्याधुनिक तकनीक है? या क्या यह सस्ते श्रम का लाभ उठाने वाली तकनीक है? ये सच है कि इनमें से कई कंपनियां जॉब क्रिएटर होने का दावा करती हैं और वे सच में ही हजारों लोगों को काम देती भी हैं। लेकिन अगर हम आत्मनिरीक्षण करें तो पाएंगे कि जो हो रहा है, वह वास्तव में भारत को तकनीक के मामले में सबसे आगे नहीं रख रहा है। यह केवल एक ऐसे अवसर का दोहन कर रहा है, जो मौजूद है। बहुत सारे गरीब लोगों को काम चाहिए और बहुत सारे अमीर लोगों को सुविधा । यही कारण है कि बड़ी तादाद में गरीब दिनभर अमीरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए दौड़ते रहते हैं। लेकिन यह कोई ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजी नहीं है। यही कारण है कि पीयूष गोयल ने भारत की टेक फर्मों से जो ऊंचे लक्ष्य रखने का आग्रह किया है, वह वाजिब है। हां, हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी में माहिर हैं, लेकिन हम आज भी बड़े पैमाने पर, कॉमर्शियल इनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं।
Date: 15-04-25
अमेरिका और चीन भारत की बढ़ती ताकत को जानते हैं
मिन्हाज मर्चेंट, ( लेखक, प्रकाशक और सम्पादक )
आईएमएफ के अनुसार, 2025 के अंत तक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं, 2027 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा और केवल अमेरिका और चीन से पीछे होगा। भारत के आलोचक हमें लगातार बताते हैं कि भारत अब भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 3,000 डॉलर है। तो हमें बढ़ती जीडीपी से क्यों खुश होना चाहिए?
सबसे पहले तो यह कि प्रति व्यक्ति आय ( पर कैपिटा इनकम) को विनिमय दरों के कारण ठीक से समझा नहीं जा सकता, इसलिए आईएमएफ देशों के बीच जीवनयापन की लागतों और वेतनमान में व्यापक अंतर को ध्यान में रखते हुए क्रय-शक्ति समता (पर्चेसिंग पॉवर पैरिटी या पीपीपी) का उपयोग करता है। इसीलिए जहां विनिमय दरों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय भारत के लिए 3,000 डॉलर और चीन के लिए 14,000 डॉलर है, वहीं पीपीपी पर यह भारत के लिए 12,000 डॉलर और चीन के लिए 22,000 डॉलर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच प्रति व्यक्ति आय के अनुपात के में अंतर घटकर 2:1 से भी कम हो जाता है।
इसका यह मतलब नहीं है कि भारत में गरीबी नहीं है। लेकिन ब्रिटिश राज के बाद 1947 में जहां गरीबी की दर 80% थी, वहीं वह अब 8% रह गई है। हालांकि भारत जैसे बड़े देश में गरीबी की 8% दर का मतलब यह है कि लगभग 12 करोड़ भारतीय आज भी रोज कमाकर खा रहे हैं। ऐसे में गरीबी को खत्म करने का एकमात्र तरीका अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाना है। ट्रम्प के टैरिफ युद्ध ने चीजों को जटिल बना दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की राह पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन इन ट्रेड सम्बंधी व्यवधानों ने अस्थायी मंदी की चिंताएं पैदा कर दी हैं। सरकार के आलोचक वैश्विक आर्थिक संकट का इस्तेमाल भारत की भविष्य की संभावनाओं को खारिज करने के लिए करते हैं। लेकिन विदेशी अर्थशास्त्री ऐसा नहीं सोचते ।
कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर जैफ्री सैक्स ने हाल ही में कहा कि अधिकांश भारतीय भारत की वास्तविक आर्थिक और भू-राजनीतिक क्षमता को नहीं समझते हैं। भारत सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी या दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जब तक कि अंग्रेज नहीं आए। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में गरीबी आई थी। सुधार धीमा और रुक-रुक कर हुआ, खासकर नेहरू- इंदिरा के समाजवादी युग में वास्तविक आर्थिक सुधार 1991 में नरसिंह राव और मनमोहन सिंह के साथ शुरू हुए। अब अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर ने भारत के लिए नई भू-राजनीतिक खिड़की खोल दी है। वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों ही भारत को अपने पक्ष में चाहते हैं, जो 2030 तक दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं- अमेरिका, चीन और भारत के बीच शक्ति के त्रिकोण के रूप में विकसित हो जाएगा।
इन मायनों में भारत एक स्विंग स्टेट है। चीन ने भारतीय निवेशकों को लुभाना शुरू कर दिया है। अमेरिका 21 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा चिलुकुरी को चार दिवसीय यात्रा पर भारत भेज रहा है। भारत को अब अपने पत्ते समझदारी से खेलने चाहिए। चीन को लेकर भारत सतर्क है। उसने चीनी विदेश मंत्री वांग यी की इस टिप्पणी का स्वागत किया है कि ‘ड्रैगन (चीन) और हाथी (भारत) को साथ मिलकर नृत्य करना चाहिए।’ लेकिन नई दिल्ली को इस बात की चिंता है कि चीन भारत में अपने वो सस्ते सामान डम्प कर रहा है, जिन्हें वह अमेरिका में नहीं बेच सकता।
अमेरिका से हमारे रिश्ते भी पेचीदा हैं। अमेरिका भारत का इस्तेमाल चीन को पछाड़ने के लिए करना चाहता है। ऐसे में भारत को अमेरिका का मोहरा नहीं बनना चाहिए। भारत के नीति-निर्माता जानते हैं कि एक महान शक्ति के रूप में पहचाने जाने के लिए उसके पास न केवल सैन्य क्षमता होनी चाहिए, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर पेश करने की क्षमता और इच्छाशक्ति भी होनी चाहिए। अब तक भारत क्वाड जैसे बहुपक्षीय सुरक्षा गठबंधनों का हिस्सा बनकर संतुष्ट रहा है। लेकिन हमें हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे भी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए।
पीपीपी के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय के आगामी दस वर्षों में दोगुनी होकर 24,000 डॉलर हो जाने का अनुमान है। 2035 तक तो दुनिया एक बहुत ही अलग जगह पर होगी और नई दिल्ली के पास भू-राजनीतिक सुई को अपनी मनचाही दिशा में मोड़ने की शक्ति होगी। अमेरिका और चीन दोनों ही यह अच्छी तरह से जानते हैं।
Date: 15-04-25
उचित सुझाव
संपादकीय
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा बदलते वक्त्त और उभरती चुनौतियों के बावजूद आज भी प्रासंगिक है। इस कार्यक्रम के लागू होने के बाद लाखों मजदूरों को काम मिला। पलायन में काफी हद तक कमी आई। मनरेगा ने साबित किया कि भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वह आज भी उम्मीद की किरण है। इस कार्यक्रम से लाखों अकुशल श्रमिकों और महिलाओं को पूरे वर्ष में सौ दिन के रोजगार की गारंटी मिली। इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए। यही वजह है कि इस कार्यक्रम में काम के दिन बढ़ाने की मांग अक्सर उठती रही है। अब संसद की स्थायी समिति ने भी मनरेगा पर भरोसा जताते हुए काम के दिनों की संख्या बढ़ा कर पांच महीने यानी डेढ़ सौ दिन करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा उसने दैनिक पारिश्रमिक कम से कम चार सौ रुपए करने की सिफारिश की है। दरअसल, अभी इस कार्यक्रम के तहत मिलने वाली मजदूरी इतनी कम है कि इससे न्यूनतम जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकतीं। रोजगार योजना के लिए आबंटित राशि में लंबे समय से ठहराव पर समिति की चिंता इसी संदर्भ में है। कोई दो राय नहीं कि इसकी राशि बढ़ने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी।
हालांकि मनरेगा में वित्तीय अनियमितता की भी शिकायतें मिलती रही हैं। इसके प्रति श्रमिकों का रुझान घटने और मजदूरी देर से मिलने पर सवाल उठते रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की स्थायी समिति ने तीन साल पहले मनरेगा का विश्लेषण करते हुए कई सुझाव दिए थे। तब उस समिति ने भी इस कार्यक्रम को नया रूप देने के लिए काम के गारंटीशुदा दिनों को सौ से बढ़ा का डेढ़ सौ करने की सिफारिश की थी और सभी राज्यों में समान मजदूरी दर करने का सुझाव दिया था। अब संसद की समिति ने उन सुझावों पर एक तरह से मुहर लगाई है। अगर मनरेगा में नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी सर्वेक्षण होगा, तो इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। भविष्य में इस कार्यक्रम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें दोराय नहीं कि मनरेगा ने अपनी सार्थकता साबित की है।
Date: 15-04-25
बदलेंगे मनरेगा के नियम
संपादकीय
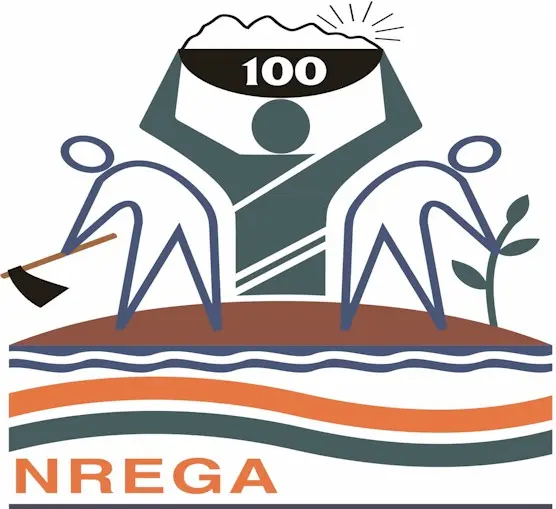 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को नई दिशा देने की कवायद एक अच्छा कदम माना जाएगा। एक संसदीय स्थायी समिति ने मनरेगा से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए और योजना को नया रूप देने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण आयोजित करने का सुझाव दिया है, जिससे मनरेगा की प्रभावशीलता का आकलन हो सकेगा। हाल ही में बजट सत्र के समापन के अंतिम हफ्ते में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने योजना के तहत काम के दिनों की संख्या को वर्तमान 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की सिफारिश की है। वहीं, समिति का सुझाव है कि मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी को कम से कम 400 रु पये प्रतिदिन तक बढ़ाया जाना चाहिए। दरअसल, मनरेगा के बजट आवंटन में पिछले कुछ वर्षों में ठहराव आया है। यहां तक कि केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार सत्तासीन होने के बाद यह आरोप भी लगा कि मोदी सरकार मनरेगा की अवधारणा को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। दो महीने पहले पेश आम बजट में ग्रामीण रोजगार योजना के लिए आवंटन 86,000 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष के समान है। इस बात को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आक्रामक रुख अपनाया। बजट के बाद कांग्रेस ने बकायदा प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया था कि इस महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच की ‘उपेक्षा’ ग्रामीण आजीविका के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाती है। बहरहाल, देश के सांसद देर से ही सही मनरेगा मजदूरों की दुदर्शा सुधारने को लेकर अगर संवेदनशील दिख रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य की सफलता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वहां सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। समग्र विकास की इस पृष्ठभूमि में मनरेगा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चूंकि मौजूदा आर्थिक मंदी ने खासतौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित किया है और रोजगार के अवसरों को काफी कम कर दिया है, इस नाते संसदीय समिति का मनरेगा को लेकर उदार और सकरात्मक कदम उठाया जाना निश्चित तौर पर मजदूर तबके के लिए राहतकारी कदम होगा। अब श्रमिकों को कार्यक्रम से अन्यायपूर्ण तरीके से बाहर नहीं किया जा सकेगा। कुल मिलाकर मनरेगा मजदूरों की दशा और दिशा सुधरने की ओर यह कदम निःसंदेह बेहतरी लाएगा।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को नई दिशा देने की कवायद एक अच्छा कदम माना जाएगा। एक संसदीय स्थायी समिति ने मनरेगा से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए और योजना को नया रूप देने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण आयोजित करने का सुझाव दिया है, जिससे मनरेगा की प्रभावशीलता का आकलन हो सकेगा। हाल ही में बजट सत्र के समापन के अंतिम हफ्ते में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने योजना के तहत काम के दिनों की संख्या को वर्तमान 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की सिफारिश की है। वहीं, समिति का सुझाव है कि मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी को कम से कम 400 रु पये प्रतिदिन तक बढ़ाया जाना चाहिए। दरअसल, मनरेगा के बजट आवंटन में पिछले कुछ वर्षों में ठहराव आया है। यहां तक कि केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार सत्तासीन होने के बाद यह आरोप भी लगा कि मोदी सरकार मनरेगा की अवधारणा को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। दो महीने पहले पेश आम बजट में ग्रामीण रोजगार योजना के लिए आवंटन 86,000 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष के समान है। इस बात को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आक्रामक रुख अपनाया। बजट के बाद कांग्रेस ने बकायदा प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया था कि इस महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच की ‘उपेक्षा’ ग्रामीण आजीविका के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाती है। बहरहाल, देश के सांसद देर से ही सही मनरेगा मजदूरों की दुदर्शा सुधारने को लेकर अगर संवेदनशील दिख रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य की सफलता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वहां सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। समग्र विकास की इस पृष्ठभूमि में मनरेगा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चूंकि मौजूदा आर्थिक मंदी ने खासतौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित किया है और रोजगार के अवसरों को काफी कम कर दिया है, इस नाते संसदीय समिति का मनरेगा को लेकर उदार और सकरात्मक कदम उठाया जाना निश्चित तौर पर मजदूर तबके के लिए राहतकारी कदम होगा। अब श्रमिकों को कार्यक्रम से अन्यायपूर्ण तरीके से बाहर नहीं किया जा सकेगा। कुल मिलाकर मनरेगा मजदूरों की दशा और दिशा सुधरने की ओर यह कदम निःसंदेह बेहतरी लाएगा।
