
08-11-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:08-11-23
Date:08-11-23
Unreal’s Reality
Deepfakes are a menace, for people, businesses, govts. But the truth is as of now the bad guys are winning
TOI Editorials
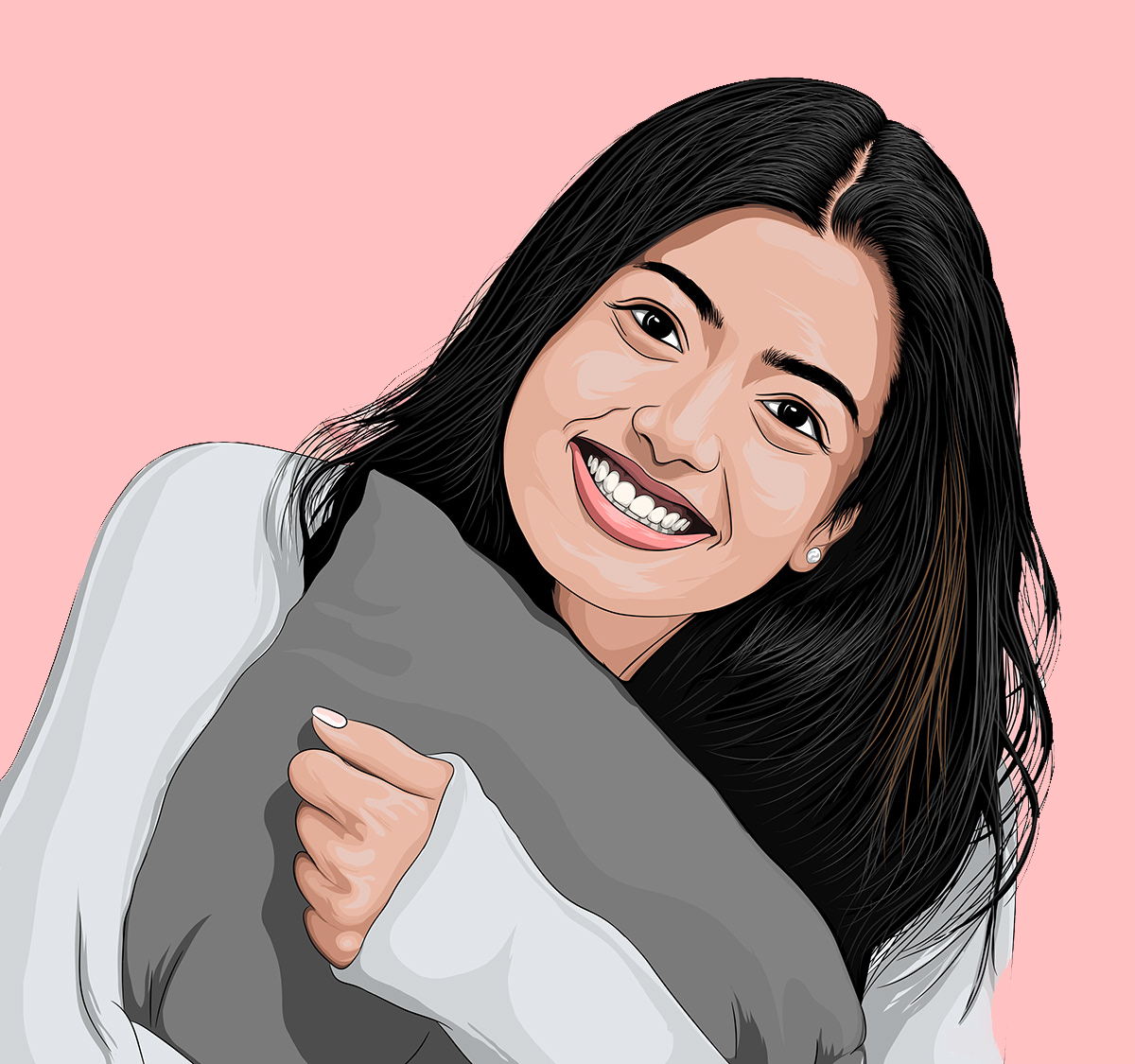
The electronics and information technology ministry has also underlined the existing rules to social media and internet companies, including IT Intermediary Rule 3(2)(b) that directs the intermediary to, within 24 hours from the receipt of a complaint, remove or disable access to the morphed content. But regulating deepfakes is a global struggle. While the US has a federal law on accountability for foreign deepfakes, a bill on defending its citizens is pending. Some US states have made nonconsensual deepfakes a criminal violation, others allow civil lawsuits. The EU is also struggling to formulate rules.
Big tech companies are responding, albeit slowly. The problem is it’s hard to detect deepfakes, as the glitches, shadows and discrepancies that visual forensics experts use to spot forgeries do not work. The tech to identify synthetic content is trailing the pace of the deepfake creators. While we wait for good tech to match up to bad tech, what do we do? Basic stuff. Be careful and complain to authorities if you are a target.
Closer together
India and Bhutan can change the development story of the region
Editorial

Efficient and time-bound execution is, therefore, key to such ambitious plans. Given India’s problems with Pakistan and sanctions on Myanmar for the 2021 coup blocking the path for trade and land connectivity to the East, working with other countries on India’s periphery to build connectivity, markets and energy links is the most sustainable way forward. In the longer term, geopolitical conflicts and anti-globalisation trends are forcing regional groupings to be more cohesive, something South Asia has not been able to achieve as yet. As India worries about China’s push into South Asian trade, infrastructure projects and strategic ties, including concerns over a Bhutan-China boundary agreement’s overhang over Doklam and India’s “Chicken Neck” (Siliguri Corridor) route, these are ideas which will offer more security and prosperity for the countries involved, with particular benefits for Bhutan, India’s traditionally trusted partner in the region.
Date:08-11-23
The problem with the ‘70 hours a week’ line
There are sound reasons why a section of India Inc. that backs the idea ought not to support a weakening of labour rights
Biswajit Dhar is a retired professor from Jawaharlal Nehru University and is now Distinguished Professor, Council for Social Development, New Delhi
The startling comment by Infosys co-founder N.R. Narayana Murthy that youngsters in India must say, “This is my country. I want to work 70 hours a week”, in order to make the country competitive, and the support he received from several members of India Inc., is undoubtedly an example of how captains of industry can adroitly hide their lust for profits by preaching virtue. More importantly, it is an argument that fails the litmus test on three counts.
First, Mr. Narayana Murthy made a factually incorrect statement that extended working hours helped advanced countries such as Germany and Japan to succeed. Second, he placed the burden of increasing productivity on the shoulders of workers, when the reality is that they have underinvested in innovation, the critical factor for raising productivity. Third, Mr. Narayana Murthy’s 70-hour week proposal violates international labour standards (ILS), the International Labour Organization’s (ILO) Decent Work Agenda and its Fundamental Conventions that lay down the working hours in order to ensure that women and men get decent and productive work. The ILS is increasingly becoming the prerequisite for gaining market access in advanced countries and for companies to participate in supply chains. Non-adherence to ILS could, therefore, seriously affect the aspirations of Indian industry to expand their presence in global markets.
Working hours in the advanced world
Contrary to Mr. Narayana Murthy’s argument, advanced countries have witnessed a continuous decline in working hours per worker during the past 150 years. In Germany, weekly working hours have reduced by about 59%, from 68 hours in 1870 to less than 28 hours in 2017. Japan had a 44-hour working week in 1961, the highest ever since 1950, which steadily decreased to less than 35 hours in 2017. Working hours tend to decrease when incomes rise and people can afford more things that they enjoy, including more leisure. In fact, in more productive economies, workers work less, while in the less productive poorer economies, workers have to work more to compensate for lower productivity.
In this context, the ILO has reminded us (“Working Time and Work-Life Balance Around the World”) that “working hours and the organization of work and rest periods can have a profound influence on the physical and mental health and well-being of workers” and that “decisions on working time issues can also have repercussions for the broader health of the economy”. In a country, i.e., India, which considers its large young workforce as its most significant asset for future development, Mr. Narayana Murthy’s pitch for a 70-hour working week is nothing but a recipe for their early burn-out.
The leading lights of India Inc. who have triggered this controversy need also to be reminded that the level of productivity of a country depends on the strength of its innovation system. India’s reality in this regard was elaborated in the India Innovation Index 2021, produced by NITI Aayog. This report showed that in 2018, India’s gross expenditure on research and development (GERD) as a percentage of GDP was 0.65%, one of the lowest in the world). This figure dipped further to 0.64% in 2020-21, according to the Department of Science and Technology (DST).
The DST also informed that the private sector’s share in the country’s R&D spending was 41% in 2020-21, a decline from 45% in 2012-13. It may be noted that in countries which have stronger innovation systems as compared to that of India’s, private sectors have much higher shares. For instance, in 2020, the private sector’s share was 79% in Japan and Korea, 75% in the United States, and 67% in Germany and the UK. Even in China, the private sector’s share was 77%. These figures cogently explain why, in general, Indian enterprises lack the competitive edge in global markets due to lower levels of productivity.
The importance of the ILS
Ironically, a section of India Inc. has supported a 70-hour working week despite being aware that if it is implemented, this would be out of step with the ILO’s Convention No. 1, the Hours of Work (Industry) Convention, 1919, which had benchmarked an eight hour average working day. Together with the ILO’s Decent Work Agenda which deals with “decent working time”, the ILS is increasingly figuring in global trade rules. Advanced countries are insisting on the inclusion of the ILS in bilateral free trade agreements (FTAs). Thus, the FTAs India is currently negotiating with the European Union (EU) and the United Kingdom, both include the ILS.
The negotiating text unveiled by the EU last year includes a chapter on Trade and Sustainable Development which says that as members of this bilateral FTA, India and the EU shall promote “decent working conditions for all, with regard to, inter alia, wages and earnings, working hours, other conditions of work and social protection”.
The ILS is also central to the implementation of the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), a 14-country grouping for promoting economic cooperation in the region led by the United States of which India is a part. Six months ago, IPEF members forged an agreement relating to supply chain resilience seeking, among other things, “to promote supply chains in which labor rights … are respected, and create market demand for sustainable and responsible sources of supply”. Labour rights, according to this agreement, includes the ILO’s Fundamental Conventions, including “acceptable conditions of work with respect to minimum wages and hours of work”. This implies that Indian companies can participate in the supply chains among IPEF members only if they respect labour rights.
Supply chain regulations
Finally, the EU member-states have put in place regulations on supply chains, the so-called “Supply Chain Due Diligence”, obliging companies to implement due diligence processes to address their adverse impact on slavery, child labour, labour exploitation, besides environmental degradation throughout across the supply chains that they participate in.
France led the way by enacting the Corporate Duty of Vigilance Law, 2017, applicable to French companies having at least 5,000 employees in France or 10,000 worldwide, either directly or in their subsidiaries. Such companies must establish a “plan of vigilance” to “identify risks and forestall serious infringements of or harm to human rights and fundamental freedoms, personal health and safety …”. Germany enacted the Supply Chain Due Diligence Act, 2022 making it mandatory for German companies with 3,000 or more employees to monitor and act on violations of human rights, including forced labour, both within their own operations, as well as those of their direct suppliers. This requirement is applicable regardless of whether the activity was performed in Germany or abroad.
Earlier this year, the EU member-states collectively adopted the Corporate Sustainability Due Diligence Directive, 2023, making it mandatory for companies to undertake due diligence to identify, and, where necessary, also prevent, end, or mitigate the negative impact of their activities on child labour and labour exploitation. Companies must assess the impact of their activities on their value-chain partners including, suppliers, sales, transport, distribution and storage.
With the developed world veering towards strict enforcement of ILS across global supply chains, India Inc. can ill-afford to support a weakening of labour rights.
संस्थाओं के आचरण से घटता भरोसा देशहित में नहीं
संपादकीय
तीन राज्य सरकारें पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने राज्यपालों के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। चौथे राज्य महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर के दल- बदल पर फैसले की टालमटोली के बाद कोर्ट को फैसले के लिए तारीखें तय करने पर मजबूर होना पड़ा। पांचवें राज्य दिल्ली में सरकार और एलजी के झगड़े में अंततः सुप्रीम कोर्ट को डीएमआरसी का चेयरमैन खुद नियुक्त करना पड़ा। उधर विधानसभा चुनावों से पहले राज्यों के चुनाव प्रचार शबाब पर हैं। इन सभी घटनाओं में एक बात समान है, वह यह है कि राज्यपाल का रवैया केवल उन्हीं राज्यों में प्रतिकारात्मक होता है, जहां विपक्षी सरकारें हैं। विधानसभाओं से पारित विधेयक पर राज्यपाल दस्तखत नहीं करते। कुलपतियों की नियुक्ति नहीं करते । संविधान के अनुच्छेद 200 यथासंभव जल्द हस्ताक्षर के प्रावधान की आड़ लेकर राज्यपाल ‘जल्द’ का मतलब ‘जब तक चाहें’ मान लेते हैं। ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कुछ ऐसी ही तस्वीर एक अन्य संवैधानिक संस्था- चुनाव आयोग के रवैये में देखने को मिलती है। वर्ष 2017 में चुनावी बॉन्ड की स्कीम घोषित करने के पहले सरकार ने महज औपचारिकता के लिए अंतिम क्षणों में राय जाननी चाही, क्योंकि कानूनी बाध्यता थी। उस समय आयोग भी इसको लेकर आश्वस्त नहीं था। लेकिन चार साल बाद वर्ष 2021 में वही चुनाव आयोग कोर्ट में इस चुनावी बॉन्ड योजना की तारीफ करता है। क्यों जनता की समझ को सत्ता के ऊंचे प्रासाद में बैठे राजनीतिक लोग इतना कम आंकते हैं?
 Date:08-11-23
Date:08-11-23
जल्द पूरा हो समझौता
संपादकीय
एक और दीवाली करीब है और भारत तथा यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौते (India-Britain FTA) पर अब तक हस्ताक्षर नहीं हो सके हैं। गौरतलब है कि एक दीवाली पहले भी इस समझौते पर हस्ताक्षर का वादा किया गया था। उम्मीद है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की दीवाली के आसपास होने वाली अचानक भारत यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। परंतु मसले इतने हैं कि यह संभावना दूर की कौड़ी नजर आ रही है। इन मसलों को देखते हुए अगर मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो भी जाते हैं तो यह बहुत हल्का और संकीर्ण होगा जबकि दोनों अर्थव्यवस्थाओं के वास्तविक एकीकरण के लिए कहीं अधिक गहन समझौते की जरूरत होगी।
इस देरी के लिए दोनों देशों के राजनीतिक और अफसरशाही प्रतिष्ठान समान रूप से उत्तरदायी हैं। भारत सरकार ने जहां एफटीए पर चर्चा करने की अपनी पुरानी अनिच्छा को बदल दिया है, वहीं अभी भी वह व्यापार से होने वाले लाभों को लेकर बहुत हिचकिचा रही है। वह विशिष्ट क्षेत्रों से झटका लगने को लेकर भी चिंतित है। यहां तक कि वे क्षेत्र जिनकी रोजगार में बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं है तथा जो अपेक्षाकृत विशेषाधिकार वाले हैं , वे भी एफटीए में देरी की वजह बनने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौतों में एक मुद्दा पेशेवर सेवाओं से जुड़े प्रश्न का भी है। भारत अपने बाजार को पेशेवर सेवाओं के लिए खोलने का इच्छुक नहीं नजर आता। खासकर विधिक सेवा जैसे क्षेत्रों में। ऐसा तब है जब इस बात पर लगातार जोर दिया जाता रहा है कि श्रमिकों की आवाजाही सभी मुक्त व्यापार समझौतों का अहम हिस्सा है। एक ओर जहां पेशेवर गिल्ड और कंपनियां बेहतर संपर्क वाली और मजबूत राजनीतिक पकड़ वाली होती हैं, वहीं यह दावा शायद ही किया जा सकता है कि उनके कारोबार पर कोई भी संभावित प्रभाव इतना गहरा होगा कि वह नए मुक्त व्यापार समझौते के सभी लाभों से परे हो। भारत सरकार को हर हितधारी समूह की बात सुननी बंद कर देनी चाहिए और अपनी नजरें अंतिम नतीजे पर रखनी चाहिए जो है: यूनाइटेड किंगडम के बाजार तक पहुंच। ध्यान रहे यूनाइटेड किंगडम अचानक अपने प्रमुख कारोबारी साझेदारों के साथ तरजीही रिश्तों से वंचित हो चुका है।
इस बीच यूनाइटेड किंगडम की सरकार राजनीतिक गतिरोधों से जूझ रही है। पिछली दीवाली तक यह समझौता पूरा करने का वादा करने वाले पिछले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बहुत पहले जा चुके हैं और उसके बाद उनकी जगह लेने वाली उदारवादी मुक्त व्यापार समर्थक लिज ट्रस भी पद से बहुत पहले हट चुकी हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री भारतीय पृष्ठभूमि के हैं। सुनक ऐसे किसी भी आरोप को लेकर काफी संवेदनशील रहेंगे कि उन्होंने भारत को कुछ ज्यादा रियायत दे दी। उनके पारिवारिक संपर्कों को देखें तो उन्हें भारत को कोई भी रियायत देने को लेकर खास सावधानी बरतनी होगी क्योंकि उसकी व्याख्या भारतीय कारोबारी जगत का पक्ष लेने के रूप में की जा सकती है। उदाहरण के लिए भारतीय आईटी कंपनियों के लिए लाभदायक हो सकने वाले अतिरिक्त वर्क वीजा सुनक के कार्यकाल में जाहिर तौर पर अधिक विवादित होंगे, बनिस्बत कि जॉनसन या ट्रस के कार्यकाल की तुलना में। खेद की बात यह है कि समय तेजी से बीत रहा है। अगर भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त समझौता अगले कुछ सप्ताह में नहीं निपटाया गया तो उसे अगले कुछ महीनों के लिए टालना पड़ सकता है। भारत में अगले वर्ष के आरंभ में आम चुनाव होने हैं और लगता नहीं है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के अंतिम कुछ महीनों में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। परंतु तब यूनाइटेड किंगडम में भी चुनाव करीब होंगे और ऐसे में सुनक के लिए भी बाजार संबंधी कोई साहसी कदम उठाना मुश्किल होगा। इस गंवाए अवसर के लिए किसी एक व्यक्ति या संस्थान को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। परंतु भारतीय कंपनियां और कर्मचारियों को एक ऐसे देश तक पहुंच गंवाने का खेद हो सकता है जो नए कारोबारी साझेदारों को लेकर उत्साहित है।
Date:08-11-23
चीन और भूटान की दोस्ती भारत के लिए नई चुनौती!
हर्ष वी पंत और आदित्य गौड़ारा शिवमूर्ति, लेखक क्रमश: ओआरएफ में उपाध्यक्ष-अध्ययन, और दक्षिण एशिया के एसोसिएट फेलो हैं
अक्टूबर में चीन का दौरा करने वाले तांदी दोरजी भूटान के पहले विदेश मंत्री हैं। उनकी यात्रा ने दो कारणों से दुनिया भर का ध्यान आकृष्ट किया है। पहला यह कि अपनी सीमा वार्ता के 25वें दौर का समापन करके भूटान और चीन अब दशकों पुराना अपना क्षेत्रीय विवाद खत्म करने के करीब हैं।
भूटान के विदेश मंत्री की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक ‘सहयोग समझौते’ पर भी हस्ताक्षर किए जिसमें विवादित सीमाओं के परिसीमन और सीमांकन के लिए काम करने वाली एक संयुक्त तकनीकी टीम की जिम्मेदारियों और कार्यों का भी जिक्र है।
दूसरा, राजनयिक संबंधों से जुड़ी बातचीत कई मौके पर सामने आई है और यह यात्रा भी दोनों देशों के संबंध सामान्य होने के संकेत देती है। हालांकि इस घटनाक्रम को देखते हुए भारत ने एक सोची-समझी चुप्पी बनाए रखी जिससे यह आभास होता है कि वह भूटान की स्थिति को समझ रहा है और उसे इस घटनाक्रम से उसके हितों को नुकसान पहुंचने की उम्मीद नहीं है।
लेकिन यह भी संभव है कि चीन के साथ भूटान के राजनयिक संबंधों के सामान्य होने से भारत को नई चुनौतियों का सामना करना पड़े।
वर्ष 1950 के दशक में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने और बाद में भूटान के आठ आंतरिक क्षेत्रों पर कब्जा करने से चिंता बढ़ी। नतीजतन, भूटान ने अपने नए पड़ोसी चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म कर दिए। इसके अलावा भूटान पी5 देशों के साथ भी राजनयिक संबंध रखने में संकोच बरत रहा था लेकिन उसने भारत के साथ अपने विशेष संबंध को स्वीकार किया।
भूटान को तिब्बत की पांच उंगलियों का हिस्सा मानने की चीन की धारणा के चलते भी भूटान भारत के करीब आने लगा। लेकिन वर्ष 1984 में द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत के साथ चीन ने विवादित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से दो क्षेत्रों तक सीमित कर दिया जिसमें उत्तर में पसमलुंग और जकरलुंग घाटियां और पश्चिम में द्रामाना, शाखातो, सिंचुलुंगपा और लांगमार पो घाटी, याक चू और चारिथांग घाटियां तथा डोकलाम पठार भी शामिल हैं।
चीन के लिए भूटान के साथ राजनयिक संबंध बनाने और विवादों का समाधान करना एक एशियाई शक्ति के रूप में उसकी छवि के लिए अहम तो है ही, साथ ही भारत के सामने अपनी आक्रामक स्थिति में सुधार के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।
इत्तफाक से चीन ने अलग-अलग वक्त में भूटान को भयभीत करने और मनाने के साथ शांत करना जारी रखा है। संभव है कि इसी दबाव की वजह से भूटान वार्ता के मंच पर आने के लिए बाध्य हुआ।
भूटान और चीन ने 1988 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और उसी साल एक समझौते को अंतिम रूप दिया। दोनों देशों के बीच 2016 तक 24 दौर की वार्ता हुई। हालांकि, हाल के वर्षों में शीर्घ समाधान के लिए चीन सक्तेंग क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में नए दावे कर रहा है और विवादित क्षेत्रों में सीमा पार से जुड़ी घुसपैठ और बस्तियां तैयार करने को बढ़ावा दे रहा है।
ऐसे वक्त में जब भारत और चीन के संबंध बिगड़ रहे हैं तब भूटान ने चीन द्वारा धीरे-धीरे विवादित क्षेत्रों में घुसने पर रोक लगाने के लिए शीघ्र वार्ता करने पर जोर दिया है।
घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति ने भी वार्ता में तेजी लाने के लिए भूटान को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया। पुराने दौर में भूटान चीन को दो टूक जवाब दे सकता था लेकिन अब यह चीन को नई विश्व व्यवस्था के एक अपरिहार्य हिस्से के रूप में देखता है जिससे अलग नहीं रहा जा सकता है। इसी वजह से भूटान में चीन का निर्यात वर्ष 2020 के 200 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022 में 1,500 करोड़ रुपये हो गया है।
संरचनात्मक मुद्दों और अवसरों की कमी के कारण युवाओं का पलायन भी बढ़ा है जिससे सुधारों की आवश्यकता बढ़ी है। इसीलिए भूटान, चीन को सुधारों की अपनी राह के लिए आवश्यक भागीदार के तौर पर देखता है। भूटान, पूंजीगत और मशीनी वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुओं और रोजमर्रा के उपकरणों का आयात करता है और इससे संकेत मिलता है कि जैसे-जैसे भूटान वृद्धि करेगा वैसे ही चीन पर इसकी निर्भरता भी बढ़ेगी। यही कारण है कि भूटान हाल के वर्षों में विवाद को समाप्त करने और चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाने के संकेत देता रहा है।
हाल के घटनाक्रम में दिख रही तेजी के बावजूद भारत ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। यह दोनों देशों के विशेष संबंधों और भूटान की सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से जुड़ी समझ के भरोसे को दर्शाता है। आज तक भारत और भूटान के बीच बहुआयामी संबंध कायम हैं।
भारत भूटान के कुल निर्यात का लगभग 70 प्रतिशत आयात करता है और दोनों का व्यापार वर्ष 2020 के 9,400 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022 में 13,400 करोड़ रुपये हो गया है। परस्पर सौहार्दपूर्ण रिश्ते के एक महत्त्वपूर्ण घटक में पनबिजली परियोजनाओं में भारत का सहयोग और भूटान के पनबिजली निर्यात शामिल है।
इसी तरह, भारत ने भूटान की वर्तमान पंचवर्षीय योजना के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपये की सहायता की पेशकश की है। दोनों देशों के बीच करीबी सुरक्षा सहयोग वाला संबंध भी कायम है। भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल, भूटानी सैनिकों को प्रशिक्षित करता है और वर्ष 2007 का समझौता कानूनी रूप से दोनों देशों को एक-दूसरे के हितों का सम्मान करने के लिए बाध्य करता है। ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि भूटान की वार्ता से भारत के हितों को कोई नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं है।
डोकलाम के मुद्दे पर भी भूटान ने त्रिपक्षीय वार्ता पर जोर देने का रुख अपनाया है जो भारत के प्रति उसकी संवेदनशीलता के भरोसे को और मजबूत करता है। हालांकि दोनों देशों के बीच बने विशेष संबंध भूटान को भारतीय हितों के प्रति विचारशील होने के बाध्य कर सकते हैं लेकिन नई चुनौतियां भी बनने की संभावना है। सबसे पहले भारत यह देखेगा कि चीन और भूटान किस तरह विवाद वार्ता से सीमा के सीमांकन की ओर बढ़ते हैं।
इसके अलावा डोकलाम जैसे संवेदनशील क्षेत्र के मुद्दे अनसुलझे हैं और सक्तेंग क्षेत्र को लेकर नए दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में भारत यथास्थिति बदलने की चीन की क्षमता और उसके इरादे को लेकर सतर्कता बरतता रहेगा। दूसरा, भूटान अब चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करके भारत और चीन की प्रतिस्पर्द्धी गतिविधियों में प्रवेश करने वाला नया और अंतिम दक्षिण एशियाई देश होगा।
चीन ने भूटान के साथ राजनयिक संबंध बनाए जाने के बाद आर्थिक, सांस्कृतिक और नागरिकों के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों के संकेत दिए हैं। इसी तरह, चीन के मीडिया सूत्रों ने भी चीन की तीन वैश्विक पहलों को मान्यता देने और समर्थन देने के लिए भूटान की सराहना की है। इससे पता चलता है कि संबंधों के उभार के इस नए चरण में भारत और भूटान के बीच नई लक्ष्मण रेखा की भी जरूरत होगी।
नाहक रार
संपादकीय
राज्यपालों की भूमिका को लेकर अब अक्सर सवाल उठने लगे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है राज्यपालों का केंद्र सरकार की तरफ झुकाव और राजनीतिक सक्रियता। विचित्र है कि इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय को नसीहत देनी पड़ी है कि राज्यपालों को समझना होगा कि वे जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। दरअसल, पिछले हफ्ते केरल, पंजाब और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी कि राज्यपाल उनके पारित विधेयकों को लटकाए हुए हैं। यहां तक कि धन-विधेयक पर भी मंजूरी नहीं दे रहे। पंजाब सरकार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह सख्त टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपालों को यह प्रवृत्ति छोड़नी होगी कि मामला अदालत में आने के बाद ही वे विधेयकों पर मंजूरी देंगे। अदालत की यह टिप्पणी एक तरह से राज्यपाल पद की गरिमा को प्रश्नांकित करने वाली है। यह शायद पहली बार है, जब राज्य सरकारों को विधानसभा में पारित विधेयकों पर मंजूरी प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जबकि राज्यपाल इस नियम से अनजान नहीं माने जा सकते कि पारित विधेयकों पर मंजूरी को लटकाए रखने का उनका अधिकार सीमित है।
हालांकि पहले भी राज्यपाल केंद्र की मर्जी के अनुरूप और दलगत झुकाव के साथ काम करते देखे जाते थे, मगर पिछले आठ-नौ सालों में जिस तरह वे प्रकट रूप में अपने पद की गरिमा को ताक पर रखते हुए काम करते देखे जा रहे हैं, उसे लेकर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। राज्यपाल का पद संवैधानिक और एक तरह से शोभा का होता है। उसका दायित्व राज्य सरकार की सहमति और सहयोग से लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक मूल्यों की पहरेदारी करना है। मगर उनकी नियुक्ति चूंकि केंद्र सरकार करती है, इसलिए जाहिर है कि दोनों के बीच अघोषित राजनीतिक स्वार्थ का सूत्र जुड़ा होता है। प्राय: जिन राज्यों में केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें होती हैं, उनमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनावपूर्ण रिश्ते देखे जाते हैं। इससे पहले भी केंद्र के इशारे पर कई बार राज्यपाल राज्य की सरकारों को अपदस्थ कर चुके हैं। मगर बीते कुछ सालों में राज्यपाल जानबूझ कर सरकारों के कामकाज में बाधा डालने का प्रयास करते देखे जा रहे हैं। दिल्ली इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां उपराज्यपाल ने एक तरह से चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिए हैं और सरकार का हर फैसला पलटते रहते हैं।
कुछ समय पहले तक पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तो जुबानी जंग भी देखी जाती थी। राज्यपाल खुल कर दलगत बयान दिया करते थे। उनके वहां से हटने के बाद ही राज्य सरकार कुछ राहत की सांस ले सकी है। मगर पंजाब में भी वही रवैया दिखाई देता है। राज्यपाल और मान सरकार के बीच अक्सर ठनी रहती है। यहां तक कि राज्यपाल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की इजाजत नहीं दी, जिसके लिए सरकार को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। ऐसे टकराव तकरीबन हर राज्य में दिखाई देते हैं, जहां केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं। इस तरह राज्यपालों ने अपने पद की गरिमा को ही गिराया है। उनके और राज्य सरकार के बीच की सियासी तकरार के चलते आखिरकार वहां की जनता को खमियाजा भुगतना पड़ता है। अनेक विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं। जो काम संवैधानिक मर्यादा में होने चाहिए, उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय को फटकार लगानी पड़े, तो यह लोकतंत्र के लिए अफसोस का विषय है।
शीर्ष अदालत की चिंता
संपादकीय
सर्वोच्च अदालत ने विभिन्न राज्यों के राज्यपालों द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों पर कार्रवाई से परहेज और उन्हें मंजूरी देने में देरी पर सोमवार को चिंता जतलाई। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यपालों को थोड़ा आत्मावलोकन करने का सुझाव देते हुए कहा कि ऐसे मामले शीर्ष अदालत आने से पहले ही कार्रवाई की जानी चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी पीठ में शामिल थे। दरअसल, राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव नई बात नहीं है। यदि केंद्र में आरूढ़ सरकार और किसी राज्य आरूढ़ सरकार एक ही पार्टी की न हों यानी डबल इंजन की सरकार न हो तो ज्यादातर देखा गया है कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव हो जाता है। चूंकि राज्यपाल केंद्र सरकार की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसलिए उनका झुकाव केंद्र में आरूढ़ पार्टी की तरफ हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि वह पूर्व में सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े नेता रहे हों। कई दफा सेवानिवृत्त नौकरशाहों या सेवानिवृत्त सेनाधिकारियों को भी राज्यपाल के रूप में मनोनीति करवा लिया जाता है। इस प्रकार नियुक्त हुए राज्यपाल केंद्र में आरूढ़ दल की इच्छा को तरजीह देते दिखते हैं। ऐसे में राज्य में सत्तासीन किसी विरोधी दल की सरकार को बाकायदा विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल से मंजूर कराने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली और पंजाब में काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार को तो उपराज्यपाल और राज्यपाल से विधानसभा में विधिवत पारित विधेयकों को मंजूरी दिलाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी है। मौजूदा विवाद भी पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार जुड़ा है। पंजाब सरकार ने राज्यपाल बीएल पुरोहित पर विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में अनावश्यक विलंब करने का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि विधेयकों को रोकने की समय सीमा होती है, लेकिन दुखद है राज्यों की सरकारों को विधानसभा का सत्र आहूत करने तक के लिए शीर्ष अदालत में आना पड़ रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच इतनी तल्खी नहीं होनी चाहिए कि ऐसी आए। शीर्ष अदालत ने अपनी सख्त टिप्पणी में कहा है कि राज्यपाल अपनी सीमा समझें, वे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं।
राज्यपालों पर सवालों का सिलसिला
राज कुमार सिंह, ( वरिष्ठ पत्रकार )
पंजाब में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के बीच विवाद में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी राजभवनों को फिर आईना दिखाने वाली है। महाराष्ट्र प्रकरण में सर्वोच्च अदालत द्वारा स्पीकर ही नहीं, राज्यपाल के आचरण पर भी की गई टिप्पणियां ज्यादा पुरानी नहीं हैं। अब पंजाब में मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयकों को राज्यपाल द्वारा रोके जाने के खिलाफ याचिका पर प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने टिप्पणी की है कि राज्यपालों को अपनी अंतर्रात्मा में झांकने की जरूरत है। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। यह भी कि वे निर्वाचित सरकारों द्वारा विधानसभा में पारित विधेयकों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही निपटाएं। पंजाब सरकार ने 28 अक्तूबर को याचिका दायर की कि राज्यपाल जुलाई में मंजूरी के लिए भेजे गए सात विधेयकों को रोके बैठे हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। इनमें से दो विधेयकों पंजाब जीएसटी (संशोधन) विधेयक और इंडियन स्टांप (संशोधन) विधेयक को 1 नवंबर को मंजूरी दी गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद नया नहीं है। इसी साल मार्च में विधानसभा सत्र बुलाते समय भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
पंजाब विवाद पर अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी, पर यह इस तरह का इकलौता मामला नहीं है। तेलंगाना और केरल की सरकारें भी राज्यपाल द्वारा विधेयक रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। शीर्ष अदालत में याचिका के बाद ही तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने लंबित विधेयकों पर कार्रवाई की है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर आरोप है कि वह आठ विधेयकों को रोके हुए हैं, जिनमें से तीन विधेयक तो दो साल से भी पुराने हैं। तमिलनाडु में भी मुख्यमंत्री एम के स्टालिन व राज्यपाल आर एन रवि के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है।
निर्वाचित राज्य सरकारों और केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपालों के बीच टकराव कई सवाल खड़े करता है, पर उनका जवाब खोजने के बजाय अमूमन उनसे मुंह चुरा लिया जाता है। पंजाब, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में टकराव के अलावा भी ज्यादातर राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जो लोकतंत्र और संविधानसम्मत शासन के लिए शुभ नहीं है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच कटुता चरम पर दिखी। झारखंड में भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तकरार की खबरें रहती हैं। दरअसल, जिन राज्यों में केंद्र से इतर राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, वहीं ऐसी तकरार बहुत कुछ कह भी देती है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल आमतौर पर उसके अपने दल के चुनाव-पराजित अथवा बुजुर्ग राजनेता या फिर चहेते पूर्व नौकरशाह आदि होते हैं, इसलिए भी वह दूसरे राजनीतिक दल की राज्य सरकार को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते।
ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के बीच टकराव अचानक बढ़ गया है। हां, उसका स्वरूप अवश्य बदला दिखता है। अब राज्यपाल अपनी सांविधानिक शक्तियों की सुविधाजनक व्याख्या कर निर्वाचित सरकारों के कामकाज में अड़ंगे लगाते हैं, जबकि अतीत में वे सरकारों को बर्खास्त कर (अपने आकाओं की) मनपसंद सरकार बनाने की हद तक जाते रहे हैं। बहुत शुरू में यह कोशिश नजर आई कि राज्यपाल नियुक्त करते समय संबंधित राज्य सरकार को भी विश्वास में ले लिया जाए, पर वैसा अपवाद स्वरूप ही हुआ। राज्यपाल को औजार बनाकर दूसरे दलों की राज्य सरकारों को अस्थिर करने का खेल आजादी के एक दशक बाद ही शुरू हो गया था। वाकया 1958 का है, जब केरल में शिक्षा में बदलाव संबंधी आंदोलन की आड़ लेकर राज्यपाल ने वामपंथी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की विडंबना यह है कि राज्यपाल के जरिये संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर निर्वाचित राज्य सरकार को अस्थिर करने की वह घटना अपवाद के बजाय, परंपरा बन गई। 1967 में राज्यपाल धर्मवीर ने पश्चिम बंगाल में अजय मुखर्जी की बहुमत प्राप्त वामपंथी सरकार को बर्खास्त कर वहां पी सी घोष के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थित सरकार बनवा दी थी। 1977 और 1980 में तो यह जैसे म्यूजिकल चेअर गेम बन गया था। आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव में जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ हुई, तो कई कांग्रेस शासित राज्य सरकारें बर्खास्त कर राज्यपाल भी हटा दिए गए। 1980 में सत्ता में वापसी के बाद इंदिरा गांधी ने भी उसी अंदाज में हिसाब चुकता किया।
अभिनेता से राजनेता बने मुख्यमंत्री एन टी रामाराव 1984 में हार्ट सर्जरी के लिए विदेश गए, तो राज्यपाल रामलाल ने एक मंत्री एन भास्कर राव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। एनटीआर की स्वदेश वापसी के बाद जब हैदराबाद से दिल्ली तक बवाल हुआ, तब शंकर दयाल शर्मा को नया राज्यपाल बनाकर भेजा गया, और एनटीआर सरकार भी बहाल हुई। 1998 में लोकसभा चुनाव के बीच ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी अनशन पर बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में बहुमत परीक्षण का आदेश दिया, और अंतत कल्याण सिंह सरकार बहाल हुई।
ऐसे घटनाक्रम की सूची बहुत लंबी बन सकती है, जब राज्यपालों पर केंद्र के एजेंट की तरह काम कर भिन्न राजनीतिक दल की राज्य सरकार को अस्थिर कर गिराने या फिर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर बर्खास्त करने के आरोप लगे। मुख्यमंत्री राज्य में सत्ता के प्रमुख होते हैं, पर संविधान के संरक्षक की भूमिका में राज्यपाल होते हैं। दोनों को सांविधानिक सीमाओं में रहते हुए परस्पर विश्वास और सद्भाव से राज्य हित में अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना चाहिए। जब इन दो महत्वपूर्ण संस्थाओं में ही अशोभनीय टकराव नजर आए, तो शासन तंत्र और उसकी छवि प्रभावित होती ही है। परिणामस्वरूप सर्वोच्च अदालत सख्त टिप्पणियां करने को बाध्य होती है और जागरूक नागरिकों को समाजवादी नेता मधु लिमये का राज्यपाल पद ही समाप्त कर देने का सुझाव विचारणीय लगने लगता है।
