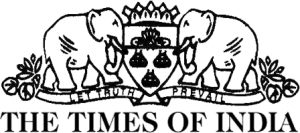01-12-2016 (Important News Clippings)
To Download Click Here
Judicial overreach
Forcing moviegoers to stand up for the national anthem won’t make them respect it
Yesterday the Supreme Court directed that the national anthem must be played before all film screenings at cinema halls across the country. And while the anthem plays, everyone in attendance must stand up to show respect. The top court reportedly said, “People nowadays don’t know how to sing national anthem and people must be taught.” This raises questions, first, about judicial overreach and second, about infantilising citizens. The job of the judiciary, including the Supreme Court, is to interpret laws and not to make them. Democracy relies on this separation of powers. But accusations of judicial overreach have become common precisely because the judiciary often usurps legislative authority.
Second, how short is the journey from mandating that everyone sing the national anthem before a movie to mandating it before every cricket match or even every commercial flight getting off the ground? This is not a silly question. It’s a serious contention that coercive nationalism demands an endless flattening of identities and behaviours. It’s offended by the rich diversity of our democracy. But nationalism should not just be something angry, punitive and authoritarian. It should also be a thing of beauty, excellence, consideration for all. The positive spirit cannot be coerced. The song dictated by force won’t be as sweet as the one that’s freely sung. When people are pressganged to show respect for the national anthem their real feelings may end up as entirely the opposite.
Finally, this court ruling comes against the backdrop of India’s great pendency of cases worsening with an eyeball to eyeball confrontation between government and judiciary. The matter of the national anthem is not urgent but is being ruled upon – while the finalisation of a new procedure to appoint judges remains in limbo.
Mixed up on movie hall nationalism

Why is the cinema seen as the right place for affirming the nation? Why not mandate that all members of any queue that is at least 15 people long sing the national anthem once every five minutes? And what is the basis for the presumption that singing Jana Gana Mana in a mechanical, perfunctory fashion just because that is a legal precondition for watching a movie would enhance the singer’s patriotic fervour? Is a symbol mere reflection of the essence? Or does it induce the essence? Will painting stripes on a dog make it a tiger? The court’s order raises a number of questions, both abstract and concrete.
Experience of citizenship is the basis of patriotism and national feeling. For that experience to be positive and affirming, social relations as mediated by the state must be such as to make citizens stakeholders in a common endeavour and individual achievements enrich the lives of society at large, vicariously, if not materially.
This can happen when policy, governance and the polity at large work to improve the lives of all and induce common stakeholdership. Then does one section’s sorrow furrow every brow and another lot’s success bring joy to all. The way to boost patriotism is to refine this politics, not to make a song and dance out of the nation’s symbols.
सिनेमाघरों में राष्ट्रगान ताकि पुरखों का बलिदान याद रहे
Date: 01-12-16
नोटबंदी को बचाकर ऐसे निकालें कालाधन

जनहित की नई सोच
आज कल मशीनें विश्व में ही नहीं, भारत में भी मनुष्यों की जगह ले रही हैं और दशकों की आर्थिक वृद्धि और जनहित की अनेक योजनाओं के बावजूद भी तीन में से एक भारतीय गरीबी रेखा के नीचे है। अधिकतर काम का मशीनीकरण होने से रोजगार में भारी मात्रा में कमी आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के मुताबिक 47 प्रतिशत नौकरियां आने वाले 20 वर्षों में ऑटोमेशन के चलते खत्म होने की कगार पर हैं। इसी प्रकार से एक ऑस्ट्रेलियाई शोध के मुताबिक तकनीक की वजह से बहुत जल्द यानी 2025 तक उनके देश में 40 प्रतिशत नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा होगा। कुछ इसी तरह के अन्य शोध ने एशिया और यूरोप के उच्च आय वाले देशों को चिंता में डाल दिया है। सिर्फ विनिर्माण के क्षेत्र में शारीरिक श्रम करने वाले लोगों की ही नौकरी खतरे में नहीं है, बल्कि दफ्तरों में काम करने वालों की नौकरियां भी जा सकती हैं, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नई सीमाएं लांघ सकती है।
यूरोप-अमेरिका की कई नामी कंपनियां रोबोट का सहारा ले रही हैं और एशियाई देशों में स्थापित अपने कारखाने बंद करने की तैयारी में हैं। जाहिर है कि यह परिदृश्य विकासशील देशों के लिए और भी अधिक चिंता की स्थिति है। अगर किसी को लगता है कि तकनीकी क्रांति के इस दौर में हमारे सस्ते मजदूरों की वजह से हम लोग अप्रभावित या कम से कम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे तो सरासर गलत होगा। विश्व बैंक ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि मशीनीकरण की वजह से चौंका देने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। भारत के सभी क्षेत्रों में 69 फीसद, चीन में 77 फीसद और इथियोपिया में 85 फीसद नौकरियों पर गंभीर खतरा है।
उन्नत तकनीक जैसे कि बिना ड्राइवर के वाहन यातायात अर्थव्यवस्था और उससे संबंधित लाखों नौकरियों को काफी बाधित करेंगे, जबकि इस बात पर मतभेद है कि कितनी जल्दी यह सब होगा। इससे संबंधित बहुत से परीक्षण चल रहे हैं और उन्हें अरबों डॉलर का आर्थिक समर्थन हासिल है। इन दिनों दुनिया के कई देशों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआइ) पर चर्चा हो रही है। यूबीआइ सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम आदर्श आर्थिक सहायता है। हालांकि लोक हितकारी राज्यों (वेलफेयर स्टेट) में इस तकनीक की जड़ें 18वीं शताब्दी में निहित हैं, लेकिन 21वी शताब्दी में यह फिर एक बार वाद विवाद का कारण बन गया है। वैसे तो यह उन देशों में ज्यादा चर्चित है जहां अधिक आय है, लेकिन आजकल भारतीय अर्थशास्त्रियों ने भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया है। विकासशील और विकसित देशों के उद्देश्य, तर्क और उपलब्ध साधनों में जमीन-आसमान का फर्क है, लेकिन हम यूबीआइ के विचार से सहमत हों या असहमत, उसकी अनदेखी नहीं कर सकते।अतीत का अनुभव यह कहता है कि हमारे राजनेताओं का पहला कदम नौकरियां बचाने के नाम पर यहां ऐसी किसी नई तकनीक का रास्ता रोकने की कोशिश होगा, लेकिन यह 1980 का वक्त नहीं है जब बैंक कंप्यूटरीकरण को संगठनों के दबाव की वजह से एक दशक तक टालना पड़ा। आज की क्रूर प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में नई तकनीक पर किसी प्रकार का प्रतिबंध बहुत कम वक्त तक ही लगाया जा सकता है और भारत को इस प्रतिस्पर्धा से बाहर रखना उसे चोटिल करने जैसा होगा।
अगर आप सोचते हैं कि यूबीआइ की वकालत सिर्फ आदर्श परिकल्पना में विश्वास रखने वाले लोग ही कर रहे हैं जिन्हें वास्तविक दुनिया का जरा भी अंदाजा नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार इस पर विचार करने वालों में पूंजीवाद में गहरा विश्वास रखने वाली सिलिकॉन वैली दौड़ में सबसे आगे है। वास्तव में वाइ कॉम्बिनेटर नाम का स्टार्टअप इनक्यूबेटर इन दिनों खूब वाहवाही बटोर रहा है और कैलिफोर्निया में एक व्यवस्थित योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो चुका है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यह विचार विकसित देशों में अपने चरम पर है। इसी साल जून के महीने में ही 2500 डॉलर प्रति माह वाली यूबीआइ योजना को अपने संविधान में लागू करने वाले संशोधन को स्विट्जरलैंड ने सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी ओर फिनलैंड प्रयोग के तौर पर ऐसी योजना लाने वाला है, जिसमें कई हजार नागरिकों को बिना किसी शर्त के मौजूदा आर्थिक सहायता के बदले 600 डॉलर प्रतिमाह दिए जाएंगे।यूबीआइ को लेकर बहस का मुद्दा यह भी है कि लोगों के काम करने के प्रति उत्साह पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस विषय पर भी मतभेद हैं कि इस गणित को विकसित और लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में कैसे इस्तेमाल में लाया जाए जिसके ऊपर जनता पर खर्च करना बड़ा बोझ है और इस खर्च में कटौती न कर पाना एक मजबूरी। इस सभी बातों पर प्रकाश डाला है अर्थ जगत की जानी-मानी पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने। उसका यही मानना है की यूबीआइ लोगों को काम करने के प्रति हतोत्साहित किए बिना गरीबी के मकड़जाल से निकालने में कामयाब होगी।
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रणब बर्धन, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विजय जोशी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मैत्रीश घटक का तो कहना है कि यूबीआइ भारत जैसे देशों के लिए और भी अधिक फायदेमंद है। इसका सीधा कारण है कि विकसित देशों में यूबीआइ फंडिंग के लिए पैसा निकालने का मतलब है गरीबों और लाचार लोगों के लिए चल रही योजनाओं पर भारी कटौती करना। भारत में ज्यादातर समाजसेवी योजनाएं गरीबों के लिए व्यर्थ की कवायद साबित हो रही हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर योजनाएं भ्रष्टाचार से भरी हुई हैं और कहीं न कहीं अमीरों के समर्थन में हैं। कॉरपोरेट टैक्स में थोड़ी कटौती और पैसे के बेजा इस्तेमाल को यूबीआइ के लिए अमल में लाना भारत के लिए वरदान साबित हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी भी इस बात का समर्थन करता है। आठ फीसद सकल घरेलू उत्पाद होने से और भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने निम्न स्तर से वापस पटरी पर आने का एक नुकसान भी हुआ है और वह यह कि अब पहले के मुकाबले रोजगार के अवसर कम पैदा हो रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में वे बढे़ थे। कई अर्थशास्त्रियों की तरह प्रोफेसर सुदीप्तो मंडल का मानना है कि यूबीआइ को लागू करने में बहुत से राजनीतिक रोड़े हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के ढांचे का आम लोगों के हित में पुन: निर्माण करना बड़े और ताकतवर वर्गों की नींव हिला देगा। हमने पहले ऐसी प्रणाली का अनुसरण करने के बहुत से अवसर गंवा दिए जो दूसरे विकासशील देशों ने अपनाए, लेकिन अब जब विकसित देशों की अर्थव्यवस्था सिमट रही है तब भारत सबसे तेजी से विकास की ओर बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन कर उभरा है। फिर भी हमारी बड़ी जनसंख्या की सारी जरूरतें तभी पूरी होंगी जब हम पारंपरिक सोच से हटकर कुछ नया सोचें।
[ लेखक बैजयंत जय पांडा, बीजद के लोकसभा सदस्य हैं ]
भारत का हीरो, क्यूबा का विलेन
कितनी स्याह और निराशाजनक दृष्टि थी यह। क्यूबा के लोग आजाद और खुश नहीं थे। चारों ओर गरीबी, औसत आधिकारिक वेतन 25 डॉलर, सरकार प्रदत्त शिक्षा, चिकित्सा और सब्सिडी वाली आवास सुविधा के बावजूद अजीब-सी स्थिति। ज्यादातर लोग याचक की स्थिति में दो या तीन तरह के काम करते दिखे, जो गैरकानूनी थे। मुंबई की मरीन ड्राइव की तरह हवाना की पहचान मालेकॉन की लंबी सड़क हर तरफ वेश्याओं से अटी पड़ी थी, जिनमें से काफी अवयस्क थीं। रात होते-होते हमारे होटल की लॉबी इनका ठिकाना बन जाती थी। यह हवाना के सबसे अच्छे होटलों में से एक था। कितनों के लिए तो उनके पिता ही ग्राहक लाने का काम करते थे।
ज्यादातर नागरिकों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। मोबाइल फोन भी पैसे वालों के पास थे। विदेशी सामान, यहां तक कि क्यूबा के कुछ अच्छे प्रोडक्ट भी आम नागरिक की पहुंच से दूर थे। द्वीप के अत्यंत चर्चित बैंड के पूर्वाभ्यास समारोह में आमंत्रित किया गया, तो मैं ड्यूटी फ्री शॉप से सात साल पुरानी लोकल रम की दो बोतलें खरीद लाया। यह देख मेरे मेजबान ने कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी, गोया मैं कोई सबसे अच्छी शैम्पेन लेकर आ गया हूं। उन्होंने ही स्पष्ट किया कि यहां के लोग तो स्थानीय स्तर पर बनने वाली अच्छी लोकल रम से भी महरूम हैं।
मैंने हवाना और सिएनफेगस दो ही शहर देखे और दोनों के बाजारों का बुरा हाल था। चारों ओर से समुद्र से घिरे और हरियाली वाले क्यूबा के बाजारों में मछली और सब्जियों का अकाल था। सरकार द्वारा संचालित रेस्तरां के खाने की तो पूछिए मत- हां, निजी भोजनालयों ‘पालदार’ में जरूर थोड़ा बेहतर खाना मिल सकता था। इन्हें पर्यटकों को ध्यान में रखकर ही अनुमति दी गई थी। मैं अवकाश पर जरूर था, लेकिन मेरे पास न्यूयॉर्क के दोस्तों के दिए गए कुछ स्थानीय फोन नंबर थे। इन्हीं में से एक से मैंने पूछा कि क्या वह कुछ आजाद ख्याल लोगों से मिलने में मेरी मदद कर सकते हैं? एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब मिला, ‘सबसे आसान तरीका तो यह है कि आप कहीं निकलें और किसी दीवार पर कास्त्रो के विरोध में कुछ लिख दें। इसके बाद पुलिस आपको जेल में ठूंस देगी… और वहां आपको बहुत सारे ऐसे आजाद ख्याल लोग अपने आप मिल जाएंगे।’
हालांकि, उन्होंने मुझे कास्त्रो से असहमत एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा दिया, जो जेल में नहीं थे। मेरा स्वागत बनावटी तिरस्कार के साथ हुआ: ‘तो आप अमेरिका से हैं। उस अमेरिका से, जो हमारी सारी मुश्किलों की जड़ है।’ यह तंज लंबे समय से चली आ रही उस सोच की ओर इशारा कर रहा था कि क्यूबा की सारी मुसीबतों के लिए साठ के दशक की शुरुआत में अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध जिम्मेदार हैं। कास्त्रो शासन ने इसे अपनी विफलताओं और भ्रष्टाचार को छिपाने का सटीक बहाना बना रखा था।
सच है कि अमेरिकी प्रतिबंधों को किसी अन्य प्रमुख देश का समर्थन नहीं मिला था, और क्यूबा के पास इस बात की तमाम संभावनाएं थीं कि वह अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध बनाता, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण हुए उसके नुकसान की भरपाई करने में मददगार साबित होते। अकेले पर्यटन क्षमता की संभावनाएं ही उसकी समृद्धि के लिए खासी मददगार साबित होतीं। जब मैं क्यूबा गया था, उसी वर्ष वहां 20 लाख से ज्यादा पर्यटक आए थे, जो इसकी एक करोड़ 20 लाख की आबादी की पर्याप्त कमाई का जरिया बन सकते थे। संदर्भवश बता दें कि एक अरब आबादी वाले भारत में उस वर्ष 55 लाख पर्यटकों की आमद दर्ज हुई थी। वहां पर्यटकों के लिए एक अलग मुद्रा की शुरुआत की गई थी, जिसका फायदा आम क्यूबाई नागरिकों तक नहीं पहुंच पाता था।
कास्त्रो के समर्थक या बचाव करने वाले वहां की शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं का हवाला देकर कास्त्रो के शासन का बखान करते हैं, लेकिन जब यही बात मैंने कास्त्रो की नीतियों से असहमत उस व्यक्ति से कही, तो उसने यह कहकर खोखली हंसी में उसको उड़ा दिया कि,‘गुलाम रखने वाला यही तर्क देगा न, कि उसके गुलाम खेती करते हुए ज्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि वहां कम से कम उन्हें भोजन और रहने का ठिकाना तो मिल जाता है। वरना अफ्रीका के जंगलों में तो शेर उन्हें मारकर खा गया होता।’ ऐसे जुमले सत्ता के खराब प्रदर्शन पर बचाव के लिए बहुत सटीक होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में क्यूबा के प्रदर्शन के ग्राफ को कैरिबियाई देशों की तुलना में देखें, तो 2009 में यह बारबडोस और एंटीगुआ-बारबुडा से पीछे खड़ा था।
बाद में तो हालत और बिगड़ी, जब यह बहामाज और ट्रिनिडाड-टोबैगो से भी पीछे चला गया। कहने की जरूरत नहीं कि यह सभी मामलों में पीछे गया, चाहे वह राजनीतिक हो, सांस्कृतिक या आर्थिक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अन्य कैरिबियाई देशों की तुलना में क्यूबा के लोग ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। काश, वे लंबी उम्र के साथ ज्यादा बेहतर जीवन भी जी रहे होते।
Cities at crossroads
Recycling begins at home

In India, the segregation of waste at source is rare. Recycling is mostly with the informal sector, although some municipalities are trying to integrate this sector into their waste management systems. More than three-fourths of the municipal budget on solid waste management goes into collection and transportation, which leaves very little for processing/resource recovery and disposal. This neglect is perhaps due to lack of awareness, in our cities, of the hugely adverse impacts of poor waste disposal on the air we breathe and the water we drink.
How else do we explain this? We still have to imbibe the basic truth that waste out of sight does not mean that it is no longer a threat to our health.
Where does waste-to-energy fit into all this? Ideally, it fits in the chain after segregation (between wet waste and the rest), collection, recycling, and before getting to the landfill, although this is not always the case. The energy from waste is a crucial element of waste management because it reduces the volume of waste for disposal and also helps in converting the waste into renewable energy and organic manure. It is not necessarily the most efficient or most economical means of generating energy.
Which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is in the waste — that is biodegradable vs non-biodegradable component — and its calorific value. The biodegradable component of India’s municipal solid waste is currently estimated at a little over 50 per cent. Biomethanation offers a major solution for processing biodegradable waste. If only we were to segregate our biodegradable waste from the rest, this could reduce the dimensions of the challenge of solid waste management to half, at one stroke.
“Biomethanation process degrades biological or organic compounds to generate biogas and manure. Biogas is a mixture containing carbon dioxide and methane in varying proportions and a small quantity of hydrogen sulfide gas. Methane is a harmful gas if released in the environment as it is one of the four major gases responsible for global warming. But it is an excellent fuel.” This is how Sharad Kale explains the phenomenon of biomethanation. He was the force behind the installation of the first biomethanation plant in Pune using nisargruna technology which was developed by him at the Bhabha Atomic Research Center, Mumbai. There are 250 biomethanation plants across India which use nisargruna technology of biomethanation. ranging in capacity from 0.25 TPD to 20.0 TPD, producing biogas and manure.
Some years ago in my column, ‘Postcards of change,’ I had written about a major initiative of decentralised biomethanation cum power generation plants in Pune. The city has taken new initiatives to try biomethanation on a medium-scale. While the decentralised small -scale biomethanation cum power generation plants have increased from 17 in 2012 to 25 in 2016 and their total capacity has increased from 83 TPD to 121 TPD, they still treat only about six per cent of the total municipal solid waste in the city.
Notwithstanding their limited share in the total waste that needs processing, the decentralised plants have made a significant contribution in solid waste management of the city in so far as they use methane as a source of renewable energy to produce electricity which is used to power street lights in surrounding areas. Not only do these plants provide a major energy saving from reduced transportation, but they also generate additional annual revenue of close to Rs 3 crore from electricity generation besides meeting their own demand for electricity.
A major new attempt at scientific management of solid waste has come forth again from Pune where the Pune Municipal Corporation and Nobel Exchange Environment Solutions, a private company have come together to commission a bio-CNG plant with a capacity to convert 300 TPD of biodegradable waste into 15,000 standard cubic meters of bio-CNG. This plant takes the process of biomethanation one step forward. Using anaerobic digestion to produce biogas and organic manure, it further processes the biogas to higher standards. The gas that is obtained can be used as an alternate fuel for natural gas vehicles or can replace other fossil fuels such as LPG/CNG and diesel.
Sources in the company indicate that the plant at present is processing 170 TPD of biodegradable waste and generating 9,000 kg of bio-CNG per day. While this is being sold as industrial fuel, the plant is also attempting to generate bio-CNG which could be used for city buses. This requires further refining of the processes to meet the necessary standards and also setting up of the requisite infrastructure with the help of the Pune Municipal Corporation.
Another medium scale initiative in biomethanation is the 400 TPD plant of Organic Recycling Systems, another private company at Solapur in Maharashtra. Based on thermophilic biomethanation process, this plant is currently accepting 200 TPD of biodegradable waste and generating 2 MW of electricity and 40 TPD of manure. The company has been awarded a contract for setting up a plant of 500 TPD capacity to process biodegradable waste in Pune.
It is too early to tell how much difference these new ventures of biomethanation will make. Will scaling-up work? In any case, the solution will only work if we are able to segregate municipal solid waste at source. Reform must begin at home.
Securing a cashless society

One of the biggest financial data breaches in India, exposed in late October, had compromised the financial data of over three million users and victimised major banking companies. The breach occurred when a network of Hitachi ATMs infected with malware enabled hackers to steal users’ login credentials and make illegal transactions. Following this, companies issued new cards and asked customers to limit their ATM usage to those operated by their banks. However, a few weeks after the breach, the demonetisation announcement pushed people to do just the opposite — rush to withdraw money from just any functioning ATM. Till date, there has been no communication from banks or the Reserve Bank of India assuring the public that the infected ATMs have been taken out of service or fixed to prevent further breaches.
Digital transactions
Over the past week, digital payments have hit record transactions: PayTM said there was a 200 per cent increase in its mobile application downloads and a 250 per cent increase in overall transactions; MobiKwik said its user traffic and merchant queries increased by 200 per cent within a few days of the government’s announcement. Companies such as Oxigen and PayU have also seen a rise in their service usage.
This trend is certainly heading in the right direction if we are moving towards a cashless economy, but the speed of technological development and its integration into our economy far supersedes the speed of defence mechanisms and protocols that could mitigate cyberattacks. Cybersecurity is unparalleled and reactive in nature, which begs the question: is it safe to utilise these new payment platforms?
PayTM, for instance, is certified under the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) 2.0 certification, which is the current industry security standard set by American Express, Visa International, MasterCard Worldwide and a few other international dealers. This is an essential certification for companies that store credit card information. PayTM and other such companies also use 128-bit encryption technology to crypt any information transfer between two systems. It takes more than a hundred trillion years to crack a password under 128-bit encryption. Needless to say, transactions via these companies are fairly secure, hence there is little doubt that companies taking advantage of demonetisation are employing their share of precautions for secure transactions.
However, this does not mean that these precautions won’t make us invulnerable. Apart from login credentials, hackers target other things. For example, just a few weeks back, hackers breached a British mobile company, Three Mobile’s database, putting at risk the private information of six million users, which was later used to purchase mobile accessories at the users’ expense. Other uses for stolen data include underground sales, identity theft, or targeted personal attacks such as extortion. According to the 2015 data breaches study by IBM and the Ponemon Institute, India is the most targeted country for data breaches.
While these attacks may appear sophisticated, there are easier methods that anyone with basic IT skills can deploy. These include creating fake mobile applications and spyware that steal information, or social engineering tactics that make you reveal your login credentials. Forums on the Internet are flush with step-by-step instructions on how to create fake websites that imitate digital payment platforms.
The larger concern, however, is that if companies like HDFC and ICICI, which are most likely proactive in updating their security systems, also experienced cyberattacks, what does that imply about unsuspecting users? Most new users, especially street vendors, have been forced onto the digital payments bandwagon. Are they aware of the security risks involved? And even if they are, what precautions can they take to minimise the potential damage from attacks?
Collective responsibility
Companies, customers, and the government should collectively participate to mitigate cyberattacks and minimise its damages.
First, all companies that offer platforms or services enabling digital payments should increase awareness among their customers of the risks, and educate them on ways to secure themselves. They must employ behaviour analytics and pattern analysis at their fraud prevention departments to predict suspicious behaviour. They must be proactive in looking out for any fake applications or websites that masquerade their service. They must monitor discussion boards, social media platforms, and forums that discuss hacking and fraud tactics, and implement measures to thwart such tactics.
Second, the government should check if the current policies regulating these platforms are adequate and update them regularly. People must be educated on the risks involved, strict policies must be enforced, and companies accountable for not meeting security standards must be held. Benefits that come from overlooking security precautions must be minimised, and public-private partnerships on live information sharing about cyberattacks and fraud should be strengthened.
Third, customers should educate themselves about the risks involved and take precautions. They must minimise vulnerability with two-factor authentication and change their password frequently. They must check the authenticity of applications by looking for the number of downloads and read reviews by other users — the higher the number of downloads and reviews, the higher the chances that the application is legitimate. Customers must also check for other application releases from that developer. For instance, they must check the Website’s authenticity by searching for the proper spelling of the Web address, check if the Website is secure by looking out for a green padlock symbol on the left side of the Web address, and keep Web browsers updated so they can recognise illegitimate sites easily.
Prime Minister Narendra Modi recently asked people to embrace the digital cashless world, reiterating that digitisation of economic activities is here to stay. In the midst of going cashless, we should not cast a blind eye to the security aspect of digital payments. We all share a collective responsibility to build a safe and secure digital infrastructure.
Puru Naidu is a research analyst with the Takshashila Institution.
Ranjeet Rane leads the digital policy team at The Dialogue, an online policy analysis portal.