
30-08-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
The Election Commission — autonomy in the crosshairs
As the focal point of differences between the government and the judiciary over its appointment procedure, the Election Commission of India is in danger of being weakened
Manjari Katju, [ teaches at the Department of Political Science, School of Social Sciences, University of Hyderabad ]

The Supreme Court of India, in a judgment on March 2, directed that the Chief Election Commissioner (CEC) and the Election Commissioners (EC) will be appointed by the President of India based on the advice of a committee made up of the Prime Minister, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha or the leader of the single largest Opposition party and the Chief Justice of India (CJI). This judgment of the Constitution Bench was a major step towards broadbasing the ECI and enhancing its constitutional status. Article 324 of the Constitution contains a provision for such a law to be enacted by Parliament.
The significance of this judgment also lies in the fact that this was a unanimous judgment of a five-judge Bench. So far, the top officers of the ECI have been appointed by the President of India on the advice of the central government. However, the government of the day, in an unambiguous move, introduced a Bill in the Rajya Sabha on August 10 which if passed will overturn this verdict.
The Bill seeks to replace the Chief Justice of India from the high-powered selection committee, meaning the committee will be made up of the Prime Minister (Chairperson), Leader of the Opposition in the Lok Sabha (Member) and a Union Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister (Member).
The government, through this Bill, has taken the Supreme Court head on, making it clear that it wants greater weightage in the appointments of the top election officials — and thus a greater hold over the institution. Experience and research show that incumbent governments, especially those with authoritarian streaks, do not usually do away with democratic institutions but, instead, relentlessly work towards making them pliant. The institutional structures remain but are drained of their substance. And, in this case, one is dealing with a matter of electoral winnability and a consolidation of state power.
An issue that has seen much debate
The procedure of appointments of the CEC and the ECs has seen much debate in policy and political circles ever since the Constituent Assembly debates and much has been written about it.
A suggestion during the Constituent Assembly Debates was that the appointment of the CEC should be subject to confirmation by two-thirds majority in a joint session of both Houses of Parliament (Constituent Assembly debates, June 15, 1949). However, Parliament was entrusted with the charge of making appropriate laws on the matter.
The V.M. Tarkunde Committee appointed by Jayaprakash Narayan in 1975, the Dinesh Goswami Committee on electoral reforms set up by the then Prime Minister, V.P. Singh, in the 1990s, and the second Administrative Reforms Commission in its fourth report in 2009 among others made recommendations that the appointments of members of the ECI should be more broad based (through a collegium) than leaving this solely to the government on whose advice the President made these appointments.
In 2006, a suggestion was made by a former CEC, B.B. Tandon, to the former President of India, A.P.J. Abdul Kalam (when both were in office) that a seven- member committee headed by the Prime Minister should choose the CEC and the other ECs. The committee should include the Lok Sabha Speaker, the Leaders of the Opposition in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, the Law Minister, the Deputy Chairperson of the Rajya Sabha and a judge of the Supreme Court nominated by the CJI. The Bharatiya Janata Party (BJP) had supported such a suggestion and argued for a representative collegium, which included the CJI to appoint the apex electoral officials. BJP General Secretary Arun Jaitley in a press release on the CPI(M)’s suggested electoral reforms in 2006 had said, ‘Any monitoring of Election Commission by Government or their nominee will be destructive of the independence of Election Commission’.
In 2012, senior leader of the BJP and former Deputy Prime Minister L.K. Advani reiterated the argument that such a collegium should be formed with the Prime Minister as its chairman, with the CJI, the Minister of Law and Justice and the Leaders of the Opposition in the Lok Sabha and the Rajya Sabha as its members. He argued that the prevalent system, whereby members to the ECI are appointed by the President, solely on the advice of the Prime Minister, does not inspire confidence among the people.
Interestingly, all these high-level committees, experienced officers and even the BJP leadership saw the importance of this and recommended that the CJI or a judge appointed by him/her should be a part of this committee; never was a suggestion made that a Union Cabinet Minister should be bestowed with this membership (and that too by replacing the CJI). In asking for reform in the appointment, the idea was to raise the ECI a few notches higher on the free and fair bar and pave the way for expunging biases and attachments to the ruling party. The effort was to curb it from becoming a ‘committed’, partisan and an incumbent-friendly entity. Through the current Bill, the government, under the BJP, is attempting to push the ECI towards further governmental control strengthening the perception about a democratic weakening.
Suggestions for reforms in the appointment procedure of the ECI came from Opposition parties, wherein the BJP was one of the most vocal parties, mainly during the Congress regime. It was felt, and rightfully so, that ruling parties have a structural advantage over institutions, making them susceptible to manipulation and biases. It was felt that having a more representative selection committee would make elections fairer by reducing the hold of the incumbent party/parties on the ECI. However, during the previous National Democratic Alliance regimes, the BJP leadership did not move on its own (clearly articulated) suggestions. Through the new Bill, it has reversed its own position which it had been voluble about while in the opposition.
Held in high regard
The ECI has been held to be a reliable, responsible and trustworthy institution by the people of India. Handling elections that involve about 900 million voters (2019 election data) through a machinery of 11 million personnel in a setting of economic hardship and inequalities is a remarkable feat. However, going soft on the ruling party or its ideology, as the perception is, whether this has to do with election schedules, electoral speeches, alleged hateful propaganda, electoral rolls or other kinds of malpractices, is eroding not only its own autonomy but also people’s trust. Nevertheless, the point remains that the present regime still sees the ECI as an institution with autonomy. And this autonomy does not gel with its goals. It would instead like a firmer grip on the ECI through statutory means.
Date:30-08-23
Gig Workers Bill: reading between the lines
Four major issues that could possibly constrict the remit and reach of the Bill
Indu Poornima is Doctoral Scholar at Centre for Public Policy, Indian Institute of Management, Bangalore; Sunny Jose is RBI Chair Professor at Council for Social Development, Hyderabad; P. Raghupathi is ICSSR Senior Fellow at Council for Social Development, Hyderabad
In a first of its kind, the Rajasthan government introduced the Rajasthan Platform-Based Gig Workers (Registration and Welfare) Bill, 2023, with the aim of ensuring social security for gig workers. Despite its good intent and noteworthy features, the Bill appears wanting in important aspects. We identify four major issues that could possibly constrict the remit and reach of the Bill.
Definitions
The first issue arises from the definitions of a gig worker and aggregator in the Bill. Drawing largely on the Code on Social Security, 2020, the Bill defines a gig worker as a ‘person who performs work or participates in a work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer-employee relationships and who works on a contract that results in a given rate of payment’. It defines an aggregator as a ‘digital intermediary… and includes any entity that coordinates with one or more aggregators for providing the services’. These definitions are far from clear and binding in treating the aggregator as employers. This lacking has a crucial bearing, as gig workers would then be seen as contractors or self-employed and not as employees by the aggregator.
Whether a gig worker and aggregator can be considered an employee and employer, respectively, has been a thorny issue globally. In fact, whether a gig worker can be considered an employee and not an independent contractor is at the core of the ABC Test. Currently integrated into California’s labour code, the test was developed as a response to a case involving delivery drivers for a same-day delivery company called Dynamex. It states that the delivery people employed by the company shall be considered as employees rather than independent contractors unless the company demonstrates that the person is free from control by the company in terms of performance of work, in deciding working hours, etc. In case it fails to do so, all the benefits meted out to a full employee of the company should be extended to the delivery workers as well. Similarly, in 2021, the U.K. Supreme Court ruled that Uber drivers must be treated as workers, and not as self-employed. This definition has been integrated under Section 230(3)(b) of the U.K. Employment Rights Act, 1996. On the contrary, the Rajasthan Bill adopts equivocal definitions amenable for conflicting interpretations, which are not only out of sync with the global best practices, but also give rise to the second but crucial issue.
Provisions
By not defining the gig workers as employees, the Bill is limited in its ability to integrate existing labour laws into its ambit. Hence, the aggregators will continue to be insulated from complying with the mandates of the labour laws, and remain evasive from the responsibility of providing the gig workers with workplace entitlements. In 2022, leading platforms in India scored zero in the Fairwork India ratings. If a gig worker is not an employee, to what extent can the aggregator be held liable for medical expenses arising from accidents at work while carrying out the work?
Agreeably, a few platforms in India do have a provision on this. But such an approach runs the risk of converting crucial entitlements like occupational safety into benevolence on the part of the aggregator. In this regard, Australia and New Zealand have brought about key changes in their laws where the vocabulary no longer surrounds ‘employer’ or ‘employee’, but rather ‘a person conducting a business or undertaking (PCBU)’ and a ‘worker in their workplace’. The onus is on the PCBU to ensure the health and safety of the worker while at the workplace or anywhere else while working.
Third, the Bill aims to create a database of gig workers wherein the details of all the workers onboarded or registered with a platform would be transferred to the proposed gig workers’ welfare board. Such a database maintained by the board does not withstand ‘the duration or time of engagement with app-based platforms’. In other words, whether the workers continue to be with the platform or not, the registration is valid for ‘perpetuity’. This progressive element might become an unintended impediment. A worker often works for two or more aggregators on a given day. Would a mandatory system of registration enable the aggregators to get to know about the worker’s details of employment with multiple aggregators and come out with mechanisms that impair the opportunity choices before the gig worker? The Bill has no preventive mechanism in this regard.
Fourth, the Bill at its core aims to guarantee social security to platform-based gig workers by constituting a representative welfare board and creating a welfare fund. It brings in eight aggregators or primary employers-based services under its remit. Yet, it neither defines categorically what constitutes social security nor specifies welfare measure that can broadly be construed as social security. Instead, it leaves this crucial aspect to the discretion of the welfare board, to ‘formulate and notify schemes for social security of registered platform-based gig workers and take such measures as it may deem fit for administering such schemes’. Though the board will have five gig worker representatives nominated by the State government, how much say they will have in the presence of vastly powerful representatives from the platforms, bureaucracy, and government is a moot question.
Thus, due to these shortcomings, whether the Bill can deliver what it promises appears doubtful.
 Date:30-08-23
Date:30-08-23
विश्व बैंक में सुधार आवश्यक
पूनम गुप्ता, ( लेखिका एनसीएईआर की महानिदेशक हैं। उन्होंने विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों में एक-एक दशक तक काम किया है )
भारत इस वक्त जी-20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है और इसके तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में पहचाने जाने वाले बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) में सुधार वास्तव में वैश्विक स्तर के सुधार एजेंडे का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। सबसे बड़े बहुपक्षीय विकास बैंकों के रूप में विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) ऐसे सुधारों के लिए सबसे प्रमुख समूह माना जा रहा है। स्वयं में सुधार लाने में अग्रणी भूमिका निभाकर यह अन्य एमडीबी के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है। डब्ल्यूबीजी, वित्त प्रदाता, सूचनाओं का संग्रहकर्ता और एक विश्वसनीय सलाहकार जैसी तीन मुख्य अहम भूमिकाएं निभाता है। वित्त प्रदाता के रूप में इसे अपने कम आय वाले सदस्य देशों (एलआईसी) और मध्यम आय वाले देशों (एमआईसी) को ऋण देने की मात्रा के जोखिम को कम करने के साथ-साथ इसका दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है।
कम आमदनी वाले सदस्य देशों की बाजार तक पहुंच कम है। इनकी अर्थव्यवस्था का आकार छोटा और इसमें काफी अस्थिरता भी है। इन्हें प्राकृतिक आपदाओं, वैश्विक जोखिम से बचने के उपायों, वैश्विक मांग में अस्थिरता, अनिश्चित व्यापार के माहौल, व्यापार की शर्तों और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से पैदा हुई कई चुनौतियों का सामना करना होता है। ये सभी कारक उनकी कर्ज लेने की क्षमता में बाधा बनकर खड़े होते हैं। विश्व बैंक समूह को अधिक लचीलापन बरतने और कम आमदनी वाले देशों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
कम आय वाले देशों के बाहरी ऋण में आधी हिस्सेदारी एमडीबी की है लेकिन इसके बावजूद इन्हें ऋण संकट से जूझना पड़ता है। यह एमडीबी द्वारा कराए गए ऋण का बोझ उठाने में सक्षम होने से जुड़े आकलन के अध्ययन की सटीकता के बारे में सवाल उठाता है। विश्व बैंक समूह सहित जितने भी एमडीबी हैं वे नए ऋण कारोबार को हासिल करने के लिए पुरस्कृत करने को तैयार होते हैं। ताजा ऋण की स्वीकृति तभी मिल सकती है जब यह माना जाए कि देश निरंतर ऋण लेने की क्षमता रखता है। इससे अनुकूल ऋण की निरंतरता के आकलन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
इसके लिए विश्व बैंक समूह को विनिमय दर मूल्यह्रास, जलवायु जोखिम और व्यापार से जुड़ी प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियों पर विचार करते हुए कम आमदनी वाले देशों के अधिक विश्वसनीय ऋण स्थिरता आकलन करना चाहिए। कम आमदनी वाले देशों के ऋण की समग्र समीक्षा, ऋण पारदर्शिता में वृद्धि और उनके मुद्रा जोखिम को कम करना आवश्यक है। ऐसे देशों की द्विपक्षीय फंडिंग के निजी या संदिग्ध स्रोतों तक पहुंच कम की जानी चाहिए और रियायती दरों पर बहुपक्षीय फंडिंग का हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा चुनौतियों से उबरने और क्षमता बढ़ाने के साथ ही कम आमदनी वाले देशों को स्थिरता और संपन्नता की दिशा की ओर जाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इन देशों के विपरीत मध्यम स्तर की आमदनी वाले देशों की बाजार तक पहुंच होती है और वे निजी पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने में भी सक्षम हैं। लेकिन पूंजी आवक की गति में स्थिरता नहीं होती है। वैश्विक धारणा में किसी भी तरह के बदलाव से निजी पूंजी प्रवाह पर तात्कालिक रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। विश्व बैंक समूह निजी पूंजी प्रवाह के जोखिम को कम कर मध्यम स्तर की आमदनी वाले देशों की फंडिंग के दायरे को बढ़ा सकता है। इसे गारंटी, अस्थायी विनिमय या आकस्मिक ऋण की पेशकश के जरिये पूरा किया जा सकता है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) वर्तमान में आकस्मिक ऋण की पेशकश करता है, लेकिन इसे लेने वालों देशों की संख्या सीमित है क्योंकि आईएमएफ से मदद मांगने पर एक नकारात्मक छवि बनती है। विश्व बैंक समूह द्वारा दी जाने वाली मदद से ऐसी किसी नकारात्मक छवि की संभावना नहीं होती है क्योंकि आईएमएफ आर्थिक संकट के दौरान उधार देता है, जबकि विश्व बैंक समूह विकास से जुड़े कार्यों की जरूरतों के लिए ऋण देता है। परिचालन के स्तर पर देखा जाए तो यह जोखिम बीमा और गारंटी इकाई, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) के माध्यम से नवाचार को शामिल करेगा।
इसके अलावा इसे जलवायु परिवर्तन जैसी प्राथमिकताओं के लिए मध्यम स्तर की आमदनी वाले देशों को उपलब्ध कराए जाने वाले वाले वित्त में वृद्धि करनी चाहिए। भारत की जी-20 अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह ने इसको लेकर महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं।
‘नॉलेज बैंक’ के रूप में विश्व बैंक समूह के प्रदर्शन में सुधार के लिए समान रूप से बड़ी गुंजाइश मौजूद है। इस नॉलेज बैंक की परिकल्पना विश्व बैंक ऋण की गुणवत्ता बढ़ाने और विकासशील देशों के लिए सेवाओं की एक नई धारा विकसित करने के अवसर के रूप में की गई थी। इसके परिचालन बजट का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा, ज्ञान के उत्पादन और प्रसार के लिए आवंटित किया जाता है लेकिन इसके बावजूद इसकी प्रासंगिकता या प्रभाव सीमित रहा है। इसके लिए एक अलग स्वतंत्र समूह शुरू करने की आवश्यकता है जो आंतरिक संगठन और प्रोत्साहन, बाहरी जुड़ाव, सहयोग और इसके ज्ञान कार्य के प्रभाव मूल्यांकन को देखे।
डब्ल्यूबीजी की जानकारी से जुड़ा काम अक्सर विभिन्न देशों के सूचकांक से जुड़ी सूचना से संबंधित होता है। उदाहरण के तौर पर इनमें से कुछ सूचकांक जैसे कि ‘कारोबार सुगमता’ सूचकांक, कई बार अपने पक्षपातपूर्ण रवैये और अविश्वसनीयता के चलते आलोचना के घेरे में आए हैं। विश्व बैंक समूह को इससे जुड़े तर्क, इसकी प्रणाली और प्रासंगिकता पर कड़ी निगाह रखने की आवश्यकता है और उनमें ही बदलाव लाने की आवश्यकता है जो सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो। इसे अपनी शोधपरक तथा प्रमुख रिपोर्टों को देश की प्रासंगिकता के अनुरूप बनाने और इसके पहुंच के दायरे का भी आकलन करना चाहिए। भारत में इसके काम का अंदाजा एक उदाहरण से मिलता है। भारत में विकास से जुड़ी कई चुनौतियां हैं जिनमें महिला श्रम बल की निरंतर कम होती भागीदारी, विनिर्माण क्षेत्र में सुस्ती और अपने कार्यबल को न केवल भारतीय, बल्कि वैश्विक बाजारों की सेवा के लिए भविष्य के लिए तैयार करने जैसी अनिवार्यता शामिल है। विश्व बैंक समूह इन महत्त्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ी चर्चा के परिदृश्य से ही गायब है। वहीं दूसरी ओर, यह हर साल भारत में वृद्धि से जुड़े छह पूर्वानुमान प्रकाशित करता है, जिनमें से प्रत्येक एक बड़े पूर्वानुमान में त्रुटि होती है और अन्य की तुलना में भी कोई सटीकता नहीं होती है। आईएमएफ भी पहले से ही इसी तरह के पूर्वानुमान प्रकाशित करता है इसलिए विश्व बैंक के संसाधनों को किसी और दिशा में लगाया जा सकता है। एक विश्वसनीय सलाहकार के रूप में इसकी भूमिका में इसी तरह की कमियां हैं, जिसके मुताबिक इससे यह उम्मीद की जाती है कि यह विकासशील देशों के सामने आने वाले जटिल नीति विकल्पों को लेकर विभिन्न देशों के प्रासंगिक अनुभवों को साझा करे। वर्तमान विकेंद्रीकृत मॉडल में देश के कर्मचारी खुद वैश्विक चलन से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं। देश के कार्यालयों में थोड़े-बहुत विचार-विमर्श से देश-विशिष्ट से जुड़ी जानकारी नहीं बढ़ती है ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापक ज्ञान से लैस होना दूर की बात है। विश्व बैंक समूह को नीतिगत मुद्दों पर विभिन्न देशों को सलाह देने के लिए और दूसरी तरफ स्थानीय भागीदारों के साथ जुड़ने के लिए अधिक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को केंद्र में लाने की आवश्यकता है। स्थानीय संस्थान, विश्व बैंक समूह द्वारा किए गए खर्च के एक हिस्से पर काम करते हैं और इसकी प्रासंगिकता और वैधता को बरकरार रखते हुए इसके संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी से करना ही फायदेमंद होगा। विश्व बैंक समूह, एक अनूठा संस्थान है और इसके पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यह एकाधिकार वाले भाव के साथ काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे अपनी अधिक जांच, आत्मनिरीक्षण पर जोर देना चाहिए। ये सभी सुधार तभी संभव हैं जब विश्व बैंक पूरी तरह से निजी तौर पर काम करने लगे जैसा कि इसके ग्राहक देशों ने किया है।
विकासशील दुनिया के देशों ने महामारी को पीछे छोड़ते हुए काम फिर से शुरू कर दिया है वहीं विश्व बैंक समूह पिछले साढ़े तीन वर्षों से ज्यादातर वर्चुअल तरीके से काम करता रहा है। वॉशिंगटन डीसी में इसके मुख्यालय के साथ-साथ नई दिल्ली सहित इसके देश के कार्यालयों में भी यही स्थिति रही है। स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के प्रस्ताव के अनुसार जी-20 की भारत की अध्यक्षता में एमडीबी और विश्व बैंक समूह से जुड़े सुधार ऐतिहासिक परिणाम साबित हो सकते हैं।
Date:30-08-23
दल-बदल विरोधी कानून में अब बदलाव जरूरी
सियासी हलचल
बीते हफ्ते गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाओ ने अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अब माना जा रहा है कि वह फिर से राकांपा में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इन्ही कारणों से भारत के दल-बदल निरोधक कानून में संशोधन की जरूरत आ गई है।
यह कहना कमतर होगा कि अलेमाओ एक ढुलमुल राजनेता हैं। वह पहली बार साल 1989 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के सदस्य (विधायक) चुने गए थे। तीन महीने बाद ही, शायद इसलिए कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, अलेमाओ ने बगावत कर दी और प्रतापसिंह राणे की सरकार को गिरा दिया। भले ही वह 18 दिन के लिए बने, लेकिन प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के नेतृत्व में वह गोवा के पहले ईसाई मुख्यमंत्री बने।
साल 1996 में अलेमाओ यूनाइटेड गोवा डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर दक्षिणी गोवा से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे। वह फिर 1999 में कांग्रेस में लौट आए और अपनी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। वह साल 2002 के विधानसभा चुनाव में हार गए मगर साल 2004 में कांग्रेस के सांसद बन गए। उन्होंने फिर कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और साल 2007 के गोवा विधानसभा चुनाव में सेव गोवा फ्रंट पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे। बाद में कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किया और उनको मंत्री बनाया।
साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा। नहीं मिलने पर उन्होंने फिर से पार्टी छोड़ दी और कुछ ही दिनों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गए और उसके टिकट पर चुनाव लड़ा। भाजपा के प्रत्याशी से वह चुनाव हार गए और फिर उन्होंने टीएमसी से भी इस्तीफा दे दिया। साल 2016 में उन्होंने राकांपा का दामन थाम कर बेनौलिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और गोवा विधानसभा में राकांपा के इकलौते विधायक बने। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने राकांपा का तृणमूल कांग्रेस में विलय कर दिया और विधानसभा में तृणमूल के इकलौते विधायक बन गए। इकलौते राकांपा विधायक होने की वजह से उन पर दल-बदल निरोधक कानून लागू नहीं हुआ।
कई लोग कहते हैं कि अलेमाओ राजनीति के ‘आया राम गया राम’ ब्रांड का प्रमुख उदाहरण है, जो 1960 और 1970 के दशक में आम बात थी। इसके परिणामस्वरूप संविधान में संशोधन किया गया और दल-बदल निरोधक कानून (दसवीं अनुसूची) लागू हुआ।
फिर भी इससे दलबदल को सत्ता के एक महत्त्वपूर्ण तरीके के रूप में रोका नहीं जा सका है। उदाहरण के लिए, साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में बहुमत नहीं मिला। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च में लेजिस्लेटिव और सिविक इंगेजमेट इनिशिएटिव के प्रमुख चक्षु राय कहते हैं, ‘भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीएस येदियुरप्पा तीन दिन के लिए मुख्यमंत्री बने और बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जनता दल के एचडी कुमारस्वामी कांग्रेस के समर्थन से 13 महीने तक प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे। दलबदल और इस्तीफों के कारण उनकी सरकार विधानसभा में विश्वास मत हार गई, जिसके बाद उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। नतीजतन, येदियुरप्पा फिर से सत्ता में लौटे और दो साल तक प्रदेश की कमान संभाली।’ उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भी साल 2018 के अंत में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अन्य दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई। लेकिन 13 महीनों के भीतर ही कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों के बाद उनकी सरकार भी गिर गई।
चूंकि दल-बदल की सबसे अधिक मार कांग्रेस पार्टी पर ही पड़ी है इसलिए इस साल फरवरी में अपने रायपुर अधिवेशन में पार्टी ने घोषणा की कि सत्ता में लौटने पर वह दल-बदल निरोधक कानून को बदलने के लिए संविधान में संशोधन करेगी। साल 2014 के बाद से भाजपा ने बड़े पैमाने पर दलबदल कराया है। आरोप है कि भाजपा ने दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीदा है और जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को एक के बाद एक गिरा दिया है। कांग्रेस ऐसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन की बात तो कर रही है मगर क्या संशोधन करेगी, इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रही है।
लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी अचारी का कहना है कि कानून के कई पहलुओं की समीक्षा की जरूरत है। उदाहरण के लिए विलय का मुद्दा, जिसका आजकल काफी दुरुपयोग किया जा रहा है। अचारी ने कहा कि 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत, यदि विधायिका का कोई सदस्य दावा करता है कि उसकी मूल राजनीतिक पार्टी का किसी अन्य पार्टी में विलय हो गया है और वह और अन्य लोग जो पार्टी की कुल ताकत का दो-तिहाई हिस्सा हैं, उस पार्टी के सदस्य बन गए हैं तो वे सदस्यता के अयोग्य होने से बच जाएंगे। लेकिन दो-तिहाई विधायकों और मूल राजनीतिक दल दोनों को विलय के लिए सहमत होना होगा। हालांकि, इस प्रावधान की व्याख्या करने वाले हालिया अदालती फैसलों ने भ्रम को और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, गोवा विधानसभा के कांग्रेस सदस्यों के भाजपा में शामिल होने पर बंबई उच्च न्यायालय के गोवा पीठ के फरवरी 2022 के आदेश में कहा गया कि यदि दो-तिहाई विधायक किसी अन्य पार्टी में विलय करते हैं तो यह कानून के तहत विलय है और इसमें मूल राजनीतिक पार्टी के विलय की आवश्यकता नहीं होगी। इस आदेश ने दल-बदल के लिए द्वार खुले छोड़ दिए हैं।
लेकिन क्या भारत में दल-बदल विरोधी कानून केवल लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को गिराने से रोकने के लिए ही मौजूद होना चाहिए? राय का कहना है कि कानून की प्रयोज्यता सरकारों को स्थिरता प्रदान करने के लिहाज से कम है और असंतुष्ट विधायकों से निपटने में पार्टी नेतृत्व के हाथों को मजबूत करने के बारे में अधिक है। उनका तर्क है कि मौजूदा कानून के मुताबिक, अगर विधायक स्वेच्छा से किसी पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं तो उन पर उससे अलग होने का आरोप लगाया जा सकता है। राय का कहना है, ‘इससे राजनीतिक दलों को अपने सांसदों और विधायकों को विधायिका से अयोग्य घोषित करने की धमकी देकर आंतरिक असंतोष को खत्म करने की अपार शक्ति मिलती है।’ चक्षु राय कहते हैं कि यह पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर एक गंभीर बंधन है। बेशक, जब अलेमाओ की अगुआई वाली जैसी एक विधायक वाली पार्टियों की बात आती है तो यह कानून लागू नहीं होता है। हालांकि इससे अस्थिरता कम नहीं बल्कि अधिक हो सकती है। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दल-बदल निरोधक कानून की गहन जांच की जरूरत है।
अब सूर्य
संपादकीय
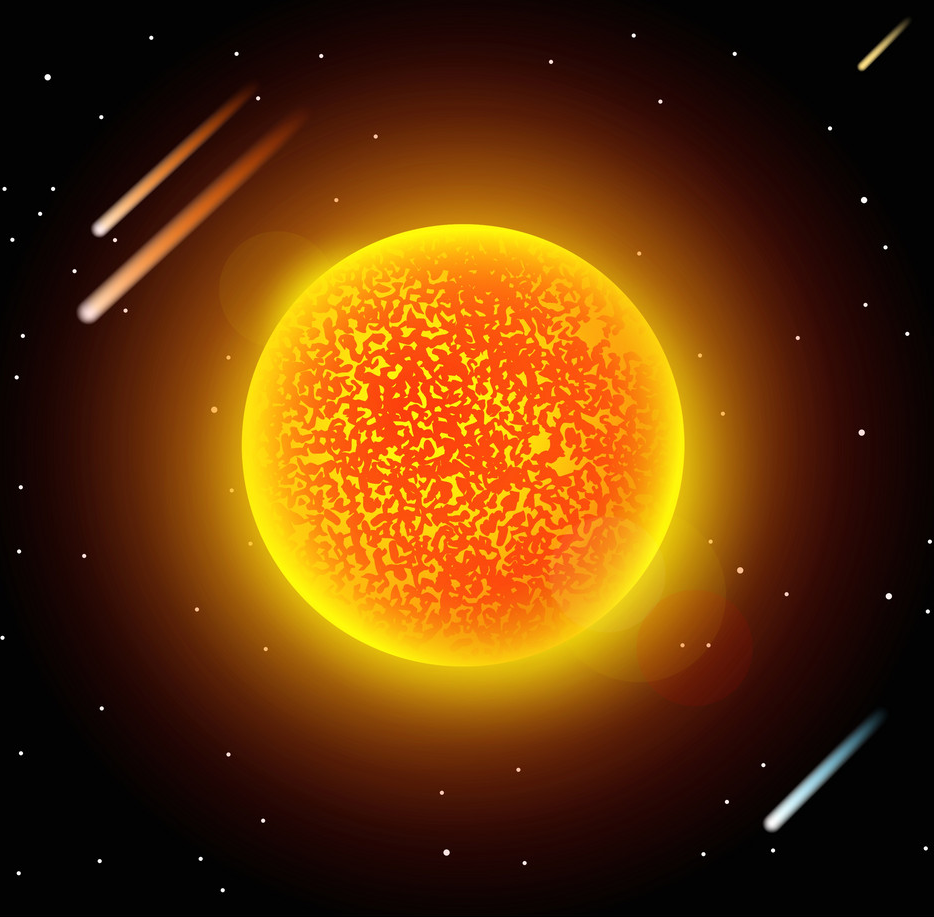
सूर्य की सतह का अध्ययन सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की अपेक्षा इसलिए कठिन माना जाता है कि वह जलती हुई गैसों का गोला है और उसके तापमान को सहन कर सकने लायक कोई धातु विकसित करना चुनौती है। मगर अत्याधुनिक दूरबीनों और तरंगमापी यंत्रों की मदद से उसकी हलचलों का अध्ययन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आदित्य-एल1 को ऐसे सात यंत्रों से लैस किया गया है। यह उस बिंदु के आसपास रह कर सूर्य की हलचलों पर नजर रखेगा, जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण और प्रतिकर्षण बल पैदा होता है। दरअसल, सूर्य का अध्ययन इसलिए भी जरूरी लगता रहा है कि सौरमंडल का यही ऐसा ग्रह है, जिसका पृथ्वी के जीवन-जगत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर सूर्य पर कोई हलचल होती है, तो उसका स्पष्ट प्रभाव पृथ्वी पर दिखने लगता है। इसलिए अब जिस तरह पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का संकट गहरा होता जा रहा है, उसमें सूर्य पर हो रही गतिविधियों का अध्ययन बहुत जरूरी हो गया है। पराबैंगनी किरणों, ओजोन परत पर सूर्य की किरणों के प्रभाव आदि की गहन जानकारी जुटाना अनिवार्य हो गया है। हालांकि पृथ्वी पर सूर्य के प्रभाव को लेकर अध्ययन हजारों वर्षों से होता आ रहा है, मगर अब उस पर हो रही हलचलों और अंतरिक्ष में आ रहे असंतुलन की वजह से पृथ्वी पर जीवन के लिए बड़े संकट की आशंका जताई जाने लगी है।
भारत से पहले अमेरिका, जर्मनी और यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बाईस बार अपने यान सूर्य मिशन पर भेज चुके हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी नासा अकेले चौदह बार अपने यान भेज चुका है। उन अध्ययनों से सूर्य को लेकर काफी कुछ बातें पता चल चुकी हैं, मगर अंतरिक्ष अध्ययन में जब तक अपने जुटाए आंकड़े न हों तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं होता। फिर हर नया अनुसंधान पिछले अनुसंधानों से आगे के बिंदुओं को केंद्र में रख कर किया जाता है। सूर्य को देखने-समझने की अपनी भारतीय दृष्टि तो है ही। अध्ययन यह भी है कि सूर्य का धीरे-धीरे क्षरण हो रहा है, जिसके चलते पृथ्वी की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वह क्षरण क्यों हो रहा है, उसे रोकने का क्या उपाय हो सकता है आदि विषयों पर भी अध्ययन होने हैं। आदित्य-एल1 से इस दिशा में बेहतर नतीजों की उम्मीद की जा रही है।
जाति-गणना के सवाल
संपादकीय
बिहार में जातिगत सर्वे का कार्य जब पूरा हो चुका है, तब इसके प्रकाशन को रुकवाने के इरादे से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के संदर्भ में केंद्र सरकार ने अपना जो पक्ष रखा है, उससे एक बार फिर जातीय गणना को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, राज्य सरकार और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति तो खैर बनी ही है। केंद्र की दलील है कि जनगणना कानून 1948 के तहत सिर्फ केंद्र सरकार जनगणना करा सकती है और दूसरी कोई संस्था यह कवायद नहीं कर सकती, वहीं बिहार सरकार का दावा है कि यह जनगणना है ही नहीं, बल्कि एक जातीय-सामाजिक सर्वे है, जो राज्य में हाशिये के लोगों के कल्याण के लिए विशेष नीति बनाने के मकसद से प्रेरित है। अब यह मामला शीर्ष अदालत में है, तो जाहिर है, उसके फैसले के बाद ही इसकी वैधानिकता अंतिम रूप से तय हो सकेगी। मगर इस पूरे प्रकरण के राजनीतिक निहितार्थ कहीं अधिक गहरे हैं।
दरअसल, बिहार और पूरे देश में धर्म व जाति की गोलबंदी में जुटी राजनीतिक पार्टियां इस गणना के सियासी नफे-नुकसान से बखूबी वाकिफ हैं और आगामी आम चुनाव में इनके इस्तेमाल का मौका वे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहतीं। इसीलिए जातीय गणना का सवाल सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस अपनी सरकार बनने की सूरत में जातिगत गणना कराने का वादा कर रही है। पिछले दिनों सागर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी स्पष्ट घोषणा की। विपक्षी दलों के महागठजोड़ ‘इंडिया’ के एजेंडे में भी यह एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। मगर 2024 के आम चुनाव को ‘मंडल बनाम कमंडल’ की पार्ट-2 लड़ाई बनाने में जुटी पार्टियों को नहीं भूलना चाहिए कि पिछले तीन दशकों में मतदाता बहुत परिपक्व हो चला है और एक के बाद दूसरे विधानसभा चुनावों में वह इसका प्रदर्शन भी कर चुका है। जातीय गणना को लेकर खड़े हुए ताजा विवाद ने राष्ट्रीय जनगणना के सवाल को भी जिंदा कर दिया है। आखिर कोरोना के कारण अपने तय समय पर न हो पाई यह जरूरी कवायद अब कब होगी? इतना तो स्पष्ट है कि अगले आम चुनाव से पहले अब यह काम संभव नहीं। ऐसे में, राज्य सरकारों के पास आधिकारिक डाटा जुटाने के लिए और क्या विकल्प बचता है?
साल 2011 की जनगणना के बाद राज्यों में काफी प्रगति हुई है और उसके आंकड़ों से तरक्की की धारा में पीछे रह गए लोगों को सही-सही लक्षित कर पाना कठिन है, जबकि उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाना राज्यों का दायित्व भी है और जरूरत भी। बेहतर होता कि जातीय गणना को सियासी फुटबॉल बनाने के बजाय एक ईमानदार कोशिश के तौर पर पेश किया जाता। जब राष्ट्रीय जनगणना में धर्मों की गिनती से हमारे सामाजिक ताने-बाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो कोई कारण नहीं कि जातियों की गिनती से अराजकता फैल जाए। जाति व समुदाय सामाजिक सच्चाई हैं, उनके आधार पर हमारे देश में आरक्षण की सांविधानिक व्यवस्था भी है। सटीक आंकडे़ इस व्यवस्था के लिहाज से भी जरूरी हैं। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक समाज लोकतंत्र की कामयाबी की पहली शर्त है। इसलिए संकीर्ण ध्रुवीकरण के नजरिये से देखने के बजाय जाति के मुद्दे को सामाजिक उत्थान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर कभी न अदालतों का वक्त जाया हो और न ही लोग किसी छलावे के शिकार बन सकें।
