
30-05-2024 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date: 30-05-24
Date: 30-05-24
Not A Drop To Waste
Water woes are a recurring Indian urban phenomenon. Reusing treated water is the solution.
TOI Editorials

The scariest moment in urban India was Chennai’s “Day Zero” in June 2019, when the city’s four major water reservoirs dried up. We are very vulnerable to water crises.
Urban mess | Common to all urban water nightmares is that economic growth and consequent building expansion have outpaced the capacity of civic authorities. Private firms have stepped into the breach to support this growth. But the downside is that they lack scale to solve critical problems.
Reality check | India cannot escape the impact of climate change. Extended heatwaves are here to stay and water demand in urban areas will not reduce. Neither can some consequences of haphazard urban expansion, such as building over natural landscapes, be undone. To illustrate, in 2022, the Karnataka govt told the state assembly that 40 lakes in Bengaluru had “disappeared”.
Recycle, the best option | On the heels of its “Day Zero”, Chennai became the first Indian city to recycle wastewater at scale. Tertiary treatment reverse osmosis plants are used to recycle water for industrial use. Recycling lifts the pressure on freshwater resources and allows urban areas to cushion the impact of poor monsoons. Some states have now mandated industrial zones to use treated water. It’s a sensible policy as India’s ranked the 13th most water-stressed in the world.
Potential’s huge | In 2016, IISc carried out a study of the potential addition to Bengaluru’s water supply through treating sewage water. It estimated that of the annual domestic demand of about 20 TMC, treated sewage could provide up to 80% of the requirement. It’s consistent with UN’s findings that on average, high-income countries treat about 70% of the industrial and municipal wastewater they generate, while the ratio falls to about 28% in lower middle-income countries.
Pushing ahead with recycling doesn’t need huge govt projects. Tight implementation of a policy to get both residential and commercial projects to use recycled water will have a significant impact. Who knows, not long after, India may go the Singapore way to use treated water in craft beer.
Human Intelligence On Keeping AI in Line
Good intent, but regulation still lacks teeth.
ET Editorials
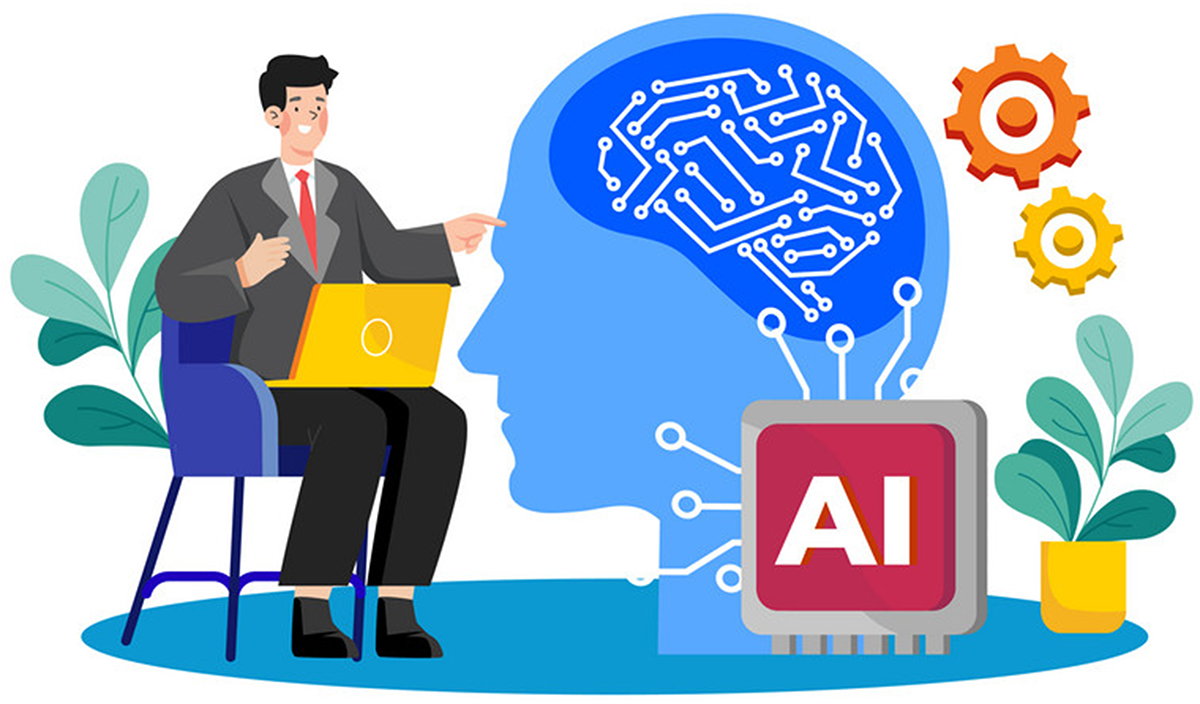
There are two ways to approach AI regulation. The first would be to apply rules to use cases. Thus, development of AI in medicine would have to conform to existing and some new regulatory conditions for the health industry. These rules can then be adjusted to fit some other industry, for instance, finance. Governments would collaborate in each of these verticals to come up with a broad set of global rules. A scaffolding, thus, emerges to keep AI within legal limits across a range of its uses. A separate set of rules would also similarly emerge on what AI should not be doing, such as its use in warfare.
The second, and much more nettlesome, approach is to control AI’s development at source. This would be in response to the risk that AI is able to independently outwit some or all use-case regulation — the Armageddon scenario. The approach to regulation here would be to control AI through computing power, over which tech creators and lawmakers differ. Governments are already prevailing by linking transparency and governance with size. Just as thresholds of ethical behaviour are being imposed on the basis of impact scale of AI deployment. All of these now await being converted into a legal harness to guide AI.
अवैध खनन का खेल
पंकज चतुर्वेदी
मई 26 को असम के तिनसुकिया जिले की पाटकाई पहाड़ियों पर अवैध रूप से संचालित ‘रेट होल माइंस’ में दब कर तीन लोग मारे गए। विदित हो पास ही मेघालय के पूर्वी जयंतिया जिले में कोयला उत्खनन की 26 हजार से अधिक ‘रेट होल माइंस’ अर्थात चूहे के बिल जैसी खदानें बंद करने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश को दस साल हो गए हैं, लेकिन आज तक एक भी खदान बंद नहीं हुई। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इन खतरनाक खदानों को बंद करने लेकिन पहले से निकाल लिए गए कोयले के परिवहन के आदेश दिए थे।
इस काम की निगरानी के लिए मेघालय हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस बीके काटके समिति ने अपनी 22वीं अंतरिम रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह ये खदानें अभी भी मेघों का देश कहे जाने वाले प्रदेश के परिवेश में जहर घोल रही हैं। उल्लेखनीय है कि कभी दुनिया में सबसे अधिक बरसात के लिए मशहूर मेघालय में अब प्यास ने डेरा जमा लिया है। यहां नदियां जहरीली हो रही हैं, और सांस में कार्बन घुल रहा है। यह सब हो रहा है इन खतरनाक खदानों से कोयले के अवैध, निर्बाध खनन के कारण। हाई कोर्ट की कमेटी बताती है कि अभी भी अकेले पूर्वी जयंतिया जिले की चूहा-बिल खदानों के बाहर 14 लाख मीट्रिक टन कोयला पड़ा हुआ है जिसको हटाया जाना है।
दस साल बाद भी इन खदानों को कैसे बंद किया जाए, इसकी ‘विस्तृत कार्यान्वयन रिपोर्ट’ अर्थात डीपीआर प्रारंभिक चरण में केंद्रीय खनन योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआई) के पास लंबित है। एक बात और, 26 हजार की संख्या तो केवल एक जिले की है, ऐसी ही खदानों का विस्तार वेस्ट खासी हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स और साउथ गारो हिल्स जिलों में भी है। इनकी कुल संख्या सात हजार से अधिक होगी। जस्टिस काटके की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘मेघालय पर्यावरण संरक्षण एवं पुनर्स्थापन निधि (एमईपीआरएफ) में 400 करोड़ रु पये की राशि बगैर इस्तेमाल पड़ी है, और इन खदानों के कारण हुए प्रकृति को नुकसान की भरपाई का कोई कदम उठाया नहीं गया। मेघालय में प्रत्येक एक वर्ग किलोमीटर में 52 रेट होल खदान हैं। अकेले जयंतिया हिल्स पर इनकी संख्या 26 हजार से अधिक है। असल में ये खदानें दो तरह की होती हैं। पहली किस्म की खदान बमुश्किल तीन से चार फीट की होती हैं। इनमें श्रमिक रेंग कर घुसते हैं। साइड कटिंग के जरिए मजूदर को भीतर भेजा जाता है और वे तब तक भीतर जाते हैं, जब तक उन्हें कोयले की परत नहीं मिल जाती। सनद रहे मेघालय में कोयले की परत बहुत पतली हैं, कहीं-कहीं तो महज दो मीटर मोटी। इसमें अधिकांश बच्चे ही घुसते हैं। दूसरे किस्म की खदान में आयताकार आकार में 10 से 100 वर्गमीटर माप में जमीन को काटा जाता है और फिर उसमें 400 फीट गहराई तक मजदूर जाते हैं। यहां मिलने वाले कोयले में गंधक की मात्रा ज्यादा है और इसे दोयम दर्जे का कोयला कहा जाता है। तभी यहां कोई बड़ी कंपनी खनन नहीं करती। ऐसी खदानों के मालिक राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, और श्रमिक बांग्लादेश, नेपाल या असम से पहुंचे घुसपैठिए होते हैं।
एनजीटी की रोक के बाद मेघालय की पिछली सरकार ने स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय आदिवासियों के अधिकार के कानून के तहत इस तरह के खनन को वैध रूप देने का प्रयास किया था लेकिन कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 के तहत कोयला खनन के अधिकार, स्वामित्व आदि हित केंद्र सरकार के पास सुरक्षित हैं। सो, राज्य सरकार अवैध खनन को वैध का अमलीजामा नहीं पहना पाई। लेकिन गैर-कानूनी खनन, भंडारण और पूरे देश में इसका परिवहन चलता रहता है। आये रोज लोग मारे जाते हैं, कुछ जब्ती और गिरफ्तारियां होती हैं, और खेल जारी रहता हैं। रेट होल खनन न केवल अमानवीय है, बल्कि इसके चलते यहां से बहने वाली कोपिली नदी का अस्तित्व ही मिट सा गया है। एनजीटी ने अपने पाबंदी आदेश में कहा था कि खनन इलाकों के आसपास सड़कों पर कोयले का ढेर जमा करने से वायु, जल और मिट्टी के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। भले ही कुछ लोग इस तरह की खदानों पर पाबंदी से आदिवासी अस्मिता का मसला जोड़ते हों, लेकिन हकीकत सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत नागरिक समूह की रिपेर्ट में बताई गई थी कि अवैध खनन में प्रशासन, पुलिस और बाहर के राज्यों के धनपति नेताओं की हिस्सेदारी है, और स्थानीय आदिवासी तो केवल शेषित श्रमिक ही हैं।
सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कोयले की कालिख राज्य की जल निधियों की दुश्मन बन गई है। लुका नदी पहाड़ियों से निकलने वाली कई छोटी सरिताओं से मिल कर बनी है, इसमें लुनार नदी के मिलने के बाद इसका प्रवाह तेज होता है। इसके पानी में गंधक की उच्च मात्रा, सल्फेट, लोहा और कई अन्य जहरीली धातुओं की उच्च मात्रा और पानी में आक्सीजन की कमी पाई गई है। एक और खतरा है कि जयंतिया पहाड़ियों के गैर-कानूनी खनन से कटाव बढ़ रहा है, दलदल बढ़ने से मछलियां कम आ रही हैं। ऊपर से जब खनन का मलबा इसमें मिलता है तो जहर और गहरा जाता है। मेघालय ने गत दो दशकों में कई नदियों को नीला होते, फिर उनके जलचर मरते और आखिर में जलहीन होते देखा है।
विडंबना है कि यहां प्रदूषण नियंतण्रबोर्ड से ले कर एनजीटी तक सभी विफल हैं। दुर्भाग्य है कि अदालत की फटकार है, पर्याप्त धन है लेकिन इन खदानों से टपकने वाले तेजाब से प्रभावित हो रहे जनमानस को कोई राहत नहीं है। यह हरियाली चाट गया, जमीन बंजर कर दी, भूजल इस्तेमाल लायक नहीं रहा और बरसात में यह पानी बह कर जब पहाड़ी नदियों में जाता है तो वहां भी तबाही ला देता है। नदी में मछलियां लुप्त हैं। मेघालय पुलिस यदा कदा अवैध कोयला की ढुलाई को लेकर मुकदमे जरूर दर्ज करती है, लेकिन ये कागजी औपचारिकता से अधिक नहीं हैं। आज जयंतिया हिल्स में असम से आए रोहिंग्या श्रमिकों की बस्तियां हैं, जो सस्ते श्रम को स्वीकार कर जान दांव पर लगा अवैध खदानों से हर रोज कोयला निकालते हैं।
अभी तो मेघालय से बादलों की कृपा भी कम हो गई है, चेरापूंजी अब सर्वाधिक बारिश वाला गांव नहीं रह गया है। यदि कालिख की लोभ में नदियां भी खोदीं तो दुनिया के इस अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य वाली धरती पर मानव जीवन भी संकट में होगा।
झुलसाती हवाओं का बढ़ता इलाका
के जे रमेश, ( पूर्व महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग )
हर साल मई के आखिरी पखवाड़े से लेकर जून के अंत तक, जब तक मानसून गंगा के मैदानी इलाकों में नहीं आ जाता, उत्तर भारत में गरमी सामान्य मौसमी परिघटना है। इन दिनों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड, बंगाल जैसे तमाम राज्य तपते रहते हैं। यह मानसून में तेजी लाने के लिए आवश्यक भी माना जाता है, क्योंकि गरमी जितनी तेज होती है, अरब सागर से उतना ही मजबूत मानसून भारत को भिगोता है। मगर अब जरूरत से अधिक गरमी पड़ने लगी है और तापमान 50 डिग्री के पार जाने लगा है। भारत के कई शहर तो पहले से अधिक गरम हो चले हैं। आखिर क्यों?
दरअसल, इसकी बड़ी वजह जलवायु में लगातार हो रहा बदलाव है। जलवायु परिवर्तन के कारण अब हर मौसम पिछला रिकॉर्ड तोड़ता नजर आता है। इसी साल जनवरी पिछले वर्ष के जनवरी माह से अधिक गरम था। फरवरी, मार्च या अप्रैल महीने की भी यही कहानी रही। स्थिति यह है कि वैश्विक गरमी 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा को पार कर चुकी है, जबकि समुद्र तटों के किनारे के देश साल 2100 तक वैश्विक गरमी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के हिमायती हैं। पेरिस समझौते में भी वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस कम करने पर सहमति बनी थी, लेकिन नतीजा अब भी सिफर ही दिख रहा है।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) का कहना है कि जब तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है, तो हीट वेव की आवृत्ति (आने की दर), समय और प्रभाव में कम से कम दोगुना का इजाफा होता है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में हीट वेव आने की दर बढ़ गई है। पहले झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्य ही इसकी चपेट में आते थे, लेकिन अब तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक जैसे इलाके भी मार्च-अप्रैल से ही बेहिसाब गरमी झेलने को मजबूर हैं। सरकारों ने तो पहले से ही इससे लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी थीं।
बहरहाल, तापमान का बढ़ना और गरमी की तपन महसूस करना, दोनों अलग चीजे हैं। आपने खबरों में भी देखा होगा कि कहीं तापमान तो कम होता है, लेकिन गरमी अधिक महसूस होती है। यह काफी हद तक नमी पर निर्भर करता है। यदि वातावरण में नमी कम हो, तो शुष्क, यानी सूखी गरमी पड़ती है, जिसमें कूलर, पंखा आदि से राहत मिल जाती है। मगर जब तापमान के साथ नमी भी होती है, तो हमारे शरीर से काफी ज्यादा पसीना निकलने लगता है और 35-36 डिग्री सेल्सियस तापमान भी 40 डिग्री के समान महसूस होने लगता है। ऐसी उमस में एयर कंडिशनर ही कारगर साबित होता है। उल्लेखनीय है कि तापमान मापने का तरीका बिल्कुल सामान्य है। शहर की कुछ जगहों पर इसकी मशीनें लगाई जाती हैं, जिनमें थर्मामीटर की तरह तापमान मापने वाला यंत्र होता है। वही हवा की गति भी माप लेता है।
अभी विशेषकर उत्तर भारत में तापमान में जो उछाल दिखने को मिल रहा है, उसमें जल्द ही कुछ राहत मिल सकती है। अगले तीन-चार दिनों में जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में तो बुधवार की शाम हल्की बारिश भी हुई। इस विक्षोभ से राजस्थान को छोड़कर शेष मैदानी इलाकों में कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, इसका असर भी तीन-चार दिनों तक ही रहेगा, फिर सूरज पहले की तरह आग बरसाने लगेगा। यह स्थिति कमोबेश मानसून आने तक बनी रहेगी।
बढ़ती गरमी मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। जिस तरह 98.5 फारेनहाइट तापमान के बाद शरीर में हलचल तेज हो जाती है, उसी तरह 37 डिग्री से अधिक का तापमान शरीर को बेचैन कर सकता है। इसके बाद मुख्यत: बेहतर प्रतिरोधक क्षमता ही गरमी का मुकाबला करती है। चूंकि बच्चे और बुजुर्गों में यह क्षमता कम होती है, इसलिए उनके साथ-साथ उन लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, जो पहले से बीमार होते हैं। हालांकि, सावधानी सामान्य आदमी को भी रखनी चाहिए, क्योंकि जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो शरीर में पानी घटने लगता है और शारीरिक क्षमता घटकर आधी रह जाती है। यही कारण है कि गरमी के महीने में पानी अधिकाधिक पीने और मौसमी फलों का सेवन करने को कहा जाता है। नारियल, खीरा, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा जैसे फल शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में सक्षम होते हैं।
एक यह सावधानी भी बरतने को कहा जाता है कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम चार बजे तक धूप के ‘एक्सपोजर’ से बचना चाहिए। महानगरों व बडे़ शहरों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) तमाम तरह के दिशा-निर्देश लागू करता है। जैसे, इस बार अस्पतालों को अपने 100 बेड लू के शिकार लोगों के लिए खाली रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बच्चों के वार्ड अस्पताल के शीर्ष तल पर न रखने के निर्देश भी हैं, क्योंकि तेलंगाना में 2017 में कई नवजातों की हुई मौत के बाद अध्ययन में यही बात सामने आई थी कि संबंधित अस्पतालों ने नवजातों को शीर्ष तल पर रखा था, जहां गरमी तुलनात्मक रूप से अधिक थी।
इसी तरह, खुले में काम करने वाले श्रमिकों, निर्माण-कारीगरों, निगम कर्मचारी, सफाईकर्मियों, कूड़ा बीनने वालों आदि को अपना काम सुबह 10 बजे तक खत्म कर लेना चाहिए और 11 बजे से चार बजे तक खुले में काम करने से बचना चाहिए। उन कंपनियों में भी दिन में छुट्टी देने की व्यवस्था की जाती है, जहां की छत गरमी से बचने के लिए नाकाफी मानी जाती है।
सवाल है कि आखिर इस बढ़ते तापमान को रोकें कैसे? इसका एक समाधान वृक्षारोपण है। इसके लिए सरकारों को आगे आना होगा। शहर में जहां हरियाली है, वहां उसे बढ़ाने की व्यवस्था करनी होगी। पार्क में वृक्षों की सघनता बढ़ानी होगी और उनकी कटाई रोकनी होगी। तापमान कम करने के लिए पार्कों के अंदर की झीलों के आसपास भी हरियाली बढ़ानी चाहिए। बेंगलुरु, हैदराबाद में तो तापमान को नियंत्रित करने के लिए रिसाइकिल वाटर, यानी दूषित जल को इस्तेमाल के लायक बनाकर पार्कों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है, इस तरह के प्रयास तमाम जगहों पर करने होंगे। एक समग्र रणनीति ही बढ़ते तापमान की तपिश से हमारी सुरक्षा कर सकती है।