
28-03-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 28-03-25
Women unbound
Public spaces must be always safe for everyone
Editorial
Despite stringent laws, women remain far from feeling safe in most public spaces. A spate of incidents in just the first three months of 2025 highlights how vulnerable women are – especially in public transport. A 23- year-old woman sustained severe injuries after jumping off a train to escape an assaulter. In another shocking case, a pregnant woman who was allegedly pushed out of a train following an attempted rape suffered a miscarriage. Harassment is a regular ordeal for women in unreserved train compartments and on government buses. Who is accountable for this grim reality when society claims to champion women’s empowerment? In their seminal work, Why Loiter?, Shilpa Phadke, Sameera Khan, and Shilpa Ranade argue that when society says it wants to protect women, it does not strive to make public spaces safer. Instead, it seeks to confine women to homes, schools, or the care of others. Even today, women must constantly consider the time of day they travel, wary of venturing out after dark or before sunrise.
A necessary starting point is affirming that wo- men have the right to live and move freely-without fear. While easier said than done, a recent Delhi High Court ruling has set an example. The court upheld the conviction of a man who sexually harassed a woman on a public bus in 2015, calling it a “deeply concerning reality” that harassment in public spaces persists despite decades of independence and tough laws. The court rightly pointed out that judgments in such cases serve as crucial signals to society. Until a harassment-free environment is created, conversations about women’s progress will remain hollow. Equally signif- icant is the Supreme Court of India’s decision to stay an Allahabad High Court order that had out- rageously ruled inappropriate touching of a mi- nor did not amount to attempted rape. The top court’s response sends a clear and much-needed message: such “totally insensitive and inhuman” interpretations of the law are unacceptable. The responsibility does not lie with the judiciary alone. Administrative bodies must ensure that streets are well-lit, police are trained to handle cases of harassment effectively, and all vacancies in law enforcement are promptly filled. Without a coordinated, all-encompassing approach to safety, women will continue to live in fear, denied their rightful access to public life.
Date: 28-03-25
नीतिगत निरंतरता की जगह भरोसे का संकट
संपादकीय
गवर्नेस जटिल प्रक्रिया है, जिसका दिशा-निर्देशन तो राजनेता कर सकते हैं, लेकिन उसके अमल को स्थायी कार्यपालिका के भरोसे ही रखना चाहिए। ट्रम्प इस सिद्धांत को धता बताते हुए अपने चुनाव में खुलकर दान देने वाले बिजनेसमैन – मित्र इलॉन मस्क से गवर्नेस की दक्षता सुधरवा रहे हैं। पिछले हफ्ते मस्क को जब पेंटागन के अधिकारियों ने चीन के बरअक्स न्यूक्लियर तैयारियों और प्रतिष्ठानों के बारे में ब्रीफ किया तो देश में भूचाल आ गया। दुनिया के लोक प्रशासन के विद्वान सकते में हैं कि बगैर पद और गोपनीयता की शपथ लिए किसी व्यक्ति को क्या अमेरिका जैसी ताकत की गुप्त जानकारियां दी जानी चाहिए? ट्रम्प-नियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वाल्ट्ज – जिनकी सेना में सेवा बहुत सीमित रही है- ने भी दो दिन पहले यमन में हूतियों पर हमले की खुफिया योजना के विवरण साझा करने के लिए बने ग्रुप में द अटलांटिक मैगजीन के सम्पादक को जोड़ लिया। मंगलवार को एक बार फिर मस्क कैबिनेट बैठक में शामिल हुए, जिससे विपक्ष नाराज है। ट्रम्प ने चार दिन पहले भारत का नाम लेकर फिर कहा था कि जैसे को तैसा टैरिफ उस पर भी लागू होगा। भारत इस मुद्दे पर वार्ता की नीति तैयार ह कर रहा था कि अब ट्रम्प ने कहा यह नीति सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होगी, ना ही सभी पर 2 अप्रैल से प्रभावी होगी। ट्रम्प-काल में नीतिगत निरंतरता की जगह भरोसे का संकट पैदा होने लगा है।
Date: 28-03-25
सेहत का मोर्चा
संपादकीय

भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के इस आकलन से अपनी पीठ थपथपा सकती है कि वर्ष 2000 के बाद भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर में 70 प्रतिशत की कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की रिपोर्ट में उन योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है, जिनके चलते शिशुओं की मृत्युदर कम करने में सफलता मिली है। इसका अर्थ है कि बीते कुछ समय में स्वास्थ्य सेवाओं और ढांचे को बेहतर करने के लिए वास्तव में कई उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। इनमें आयुष्मान भारत योजना भी है । इसका उल्लेख भी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने विशेष रूप से किया है। यह स्वास्थ्य संबंधी विश्व की सबसे बड़ी योजना है। यह निर्धन परिवारों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। आश्चर्य नहीं कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि भारत ने लाखों लोगों के जीवन को बचाने का काम किया है। आयुष्मान भारत योजना की उपयोगिता को देखकर ही हाल में 70 वर्ष की आयु के सभी बुजुर्गों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। बीते दिनों एक संसदीय समिति ने जिस तरह 60 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिकों को इस योजना के दायरे में लाने की जरूरत जताई, उससे यही इंगित होता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए न केवल केंद्र सरकार को तत्पर रहना चाहिए, बल्कि राज्य सरकारों को भी।
केंद्र और राज्य सरकारों को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्वास्थ्य ढांचा सही स्थिति में नहीं है। छोटे शहरों और गांवों में न केवल डाक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, बल्कि अस्पतालों और मेडिकल उपकरणों की भी। इसके चलते इन क्षेत्रों के लोग शहरों के बड़े अस्पतालों की ओर दौड़ लगाते हैं, जहां निजी क्षेत्र के अस्पतालों के मुकाबले सरकारी अस्पताल बहुत पीछे नजर आते हैं। यह एक हकीकत है कि एक बड़ी संख्या में लोग सरकारी अस्पतालों में मजबूरी में ही उपचार कराना पसंद करते हैं। यह सही है कि बीते कुछ वर्षों में अनेक नए मेडिकल कालेज खुले हैं, लेकिन इन मेडिकल कालेजों से निकले डाक्टर ग्रामीण इलाकों में सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं होते। समय के साथ उपचार महंगा होता जा रहा है। यदि किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को निजी अस्पताल में उपचार कराना पड़ता है तो वह कर्जे में डूब जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि अपने यहां स्वास्थ्य बीमा का उतना चलन नहीं, जितना आवश्यक है। सरकारें इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकतीं कि अधिक आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा महंगा होता जाता है और इसके बाद भी उसमें अच्छा-खासा जीएसटी लगता है। आखिर क्यों? अच्छा हो कि सरकारें सेहत के मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें।

Date: 28-03-25
उद्यमों को मिले नीतिगत समर्थन
संपादकीय
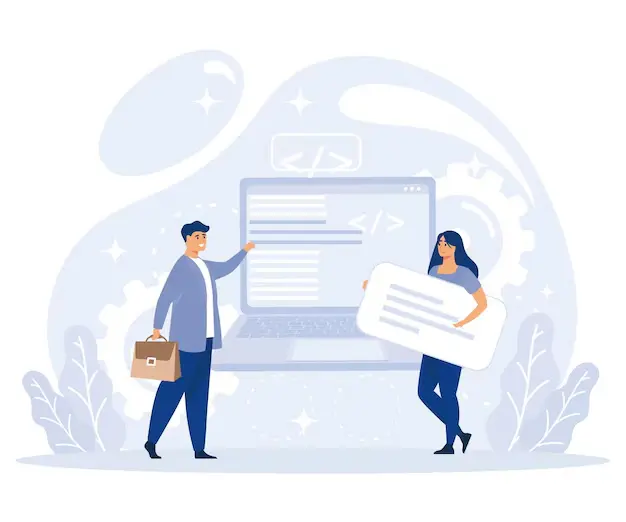
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई के सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में बढ़कर 30.1 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो 2020-21 में 27.3 प्रतिशत दर्ज हुई थी। एमएसएमई क्षेत्र से निर्यात भी बढ़ा है। इस क्षेत्र से 2020-21 में लगभग 4 लाख करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ था, जो 2024- 25 में बढ़ कर 12.39 लाख करोड़ रुपये हो गया। आर्थिक वृद्धि में एमएसएमई के योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए अनुकूल एवं उपयुक्त माहौल देना चाहिए। उन्हें अनुकूल नीतियों के जरिये समर्थन भी दिया जाना चाहिए। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने नीति फ्रंटियर टेक हब और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर बुधवार को एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म को डिजिटल एक्सीलेंस फॉर ग्रोथ ऐंड एंटरप्राइजेज वा ‘डीएक्स एज’ का नाम दिया गया है। वह प्लेटफॉर्म एमएसएमई को बदलते वक्त में प्रतिस्पद्ध बने रहने के लिए आवश्यक तकनीक एवं ज्ञान उपलब्ध कराएगा। सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर एक औद्योगिक संगठन द्वारा की गई ऐसी पहल का अवश्य स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि वे लघु एवं मझोली कंपनियों को नई तकनीक के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं।
किंतु, लघु एवं मझोली कंपनियों के समक्ष तकनीक तक पहुंच हासिल करने की ही एकमात्र चुनौती नहीं है। नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने ‘एक्स-एज’ की शुरुआत के अवसर पर कहा कि भारत में आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए पर्याप्त मझोली कंपनियां मौजूद नहीं हैं। सच्चाई तो है कि यह कोई नई समस्या नहीं है। भारत में छोटी आकार की कंपनियां बड़ी संख्या में मौजूद रही हैं किंतु उनमें अधिकांश अपना आकार या कारोबार बढ़ाने में विफल रहती हैं। वास्तव में, भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम एवं अन्य लोगों द्वारा हाल में किए गए एक शोध में निकल कर आया है कि उनमें कुछ कंपनियां बड़ी मानी जा रही थीं किंतु वास्तव में असलियत कुछ और है और वे कई संयंत्रों से संचालन कर रही थीं। इसका परिणाम यह हुआ है कि वे अपने आकार का फायदा उठाने में सफल नहीं रही हैं। विभिन्न छोटे-छोटे संयंत्रों से परिचालन करने के कई कारण रहे हैं। उनमें एक यह है कि वे कानूनी एवं राजनीतिक जोखिम कम करने के इरादे से ऐसा करती हैं। कारोबार बढ़ने के साथ ही उद्यमियों के लिए नियमों का अनुपालन करना कठिन हो जाता है।
इससे श्रम का संविदाकरण बढ़ गया है। नियामकीय बाधाओं एवं कमियों के कारण भारतीय कंपनियों को अपना आकार बढ़ाने में दिक्कत महसूस हुई है जिससे विनिर्माण जीवीए कम रहा है। इसका एक परिणाम यह भी सामने आया है कि भारतीय श्रम बल का लगभग आधा हिस्सा कृषि क्षेत्र में ही लगा हुआ है और श्रम की पर्याप्त उपलब्धता का देश को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाया है। यह तो मालूम ही है कि देश में मझोली आकार की कंपनियां अधिक नहीं है इसलिए समाधान पर भी चर्चा होती रही है। श्रम कानून इसी से जुड़ा हुआ है और नए अम कानून पारित भी हुए हैं, किंतु संबंधित हितधारकों के बीच आपसी सहमति नहीं होने के कारण वे लागू नहीं हो पाए हैं। विभिन्न स्तरों पर कानूनी एवं संचालन से जुड़ी कठिनाइयों को भी दूर करने की आवश्यकता है। संसद की लोक लेखा समिति ने इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट में एमएसएमई एवं निर्यातकों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत आ रही कठिनाइयों का उल्लेख किया है। इन मामलों का समाधान पूरी तत्परता के साथ किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में डरेगुलेशन आयोग का जिक्र किया था। ऐसा कोई आयोग अगर अस्तित्व में आता है तो इससे सरकार एवं नियामकों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्त्वहीन हो चुके एवं अनावश्यक नियम-कायदों को समाप्त करने में काफी सहायता मिल सकती है। दुनिया में बढ़ती संरक्षणवादी मानसिकता को देखते हुए वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां निकट भविष्य में अनुकूल नहीं रह सकती हैं। इसे देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में सरकार की नीति का लक्ष्य भारतीय कारोबार की राह से बाधाएं दूर करने और उन्हें आगे बढ़ने एवं प्रतिस्पद्ध बनाने पर केंद्रित होना चाहिए।
Date: 28-03-25
सवाल का जोखिम
संपादकीय
एक लोकतांत्रिक देश के संघीय ढांचे की अहम पहचान है सवाल पूछना और अभिव्यक्ति की आजादी । नागरिकों की आवाज को समाचार में जगह देना पत्रकार का दायित्व होता है। अगर वह सच्चाई सामने नहीं लाएगा, जनता की परेशानियों तथा उनकी नाराजगी को सामने नहीं रखेगा, तो पत्रकारिता अपना मूल उद्देश्य खो देगी। लेकिन देखा जा रहा है कि व्यवस्था से जुड़े लोग अपने खिलाफ कोई भी स्वर नहीं सुनना चाहते। इसकी बानगी गुवाहाटी में देखने को मिली, जहां एक सहकारी बैंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सवाल पूछने वाले पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे बाद में एक अदालत ने जमानत भी दे दी। वह पत्रकार उस बैंक में चल रही अनियमितताओं को लेकर लगातार अपने समाचार पोर्टल पर लिख रहा था। उस बैंक में ऊंचे पदों पर सत्ता से जुड़े लोग काबिज हैं। माना जा रहा है कि वह पत्रकार उन लोगों के निशाने पर था। हालांकि पुलिस का कहना है कि उस पत्रकार ने जनजातीय समुदाय के एक व्यक्ति के खिलाफ जातिवादी टिप्पणियां की थी, जिस कारण कार्रवाई की गई।
व्यवस्था के विरोध में जनता के लिए लिखने वाले पत्रकारों के प्रति शासन की असहिष्णुता की खबरें अक्सर सामने आती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कोई पत्रकार कैसे अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगा। तमाम वैश्विक एजेंसियां भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठा रही हैं। यह खेदजनक है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत लगातार नीचे खिसक रहा है। 180 देशों में भारत वर्तमान में 159 वें स्थान पर है। सूचकांक के अनुसार, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्किये और रूस के बराबर माना जा रहा है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में पत्रकारों को भारत की तुलना में ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त है, जबकि चीन और रूस निचले पायदान पर हैं। दक्षिण एशियाई देशों में, बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देश भारत से बेहतर स्थान पर हैं। हमें सोचना होगा कि हम कहां खड़े हैं। लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने वाले इस अहम कारक की ओर ध्यान देना होगा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही है जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करती है।
Date: 28-03-25
भाषाई शालीनता
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्तन छूने वाले विवादित फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था, पीड़िता के स्तन छूना और पायजामे की डोरी तोड़ने को बलात्कार या बलात्कार की कोशिश नहीं है। बेंच ने इस फैसले को पूरी तरह असंवेदनशील व अमानवीय ठहराते हुए कहा कि यह फैसला अचानक नहीं सुनाया गया है बल्कि चार माह तक सुरक्षित रखने के बाद फैसला आया है। इसका मतलब है, जज ने उचित विचार-विमर्श करके और दिमाग लगाकर यह फैसला दिया है। पीठ ने कहा ऐसे कठोर शब्दों के प्रयोग पर हमें खेद है। शीर्ष अदालत ने इस पर केंद्र व उप्र सरकार को नोटिस भी भेजा। हाईकोर्ट का यह फैसला उप्र के कासगंज के मामले में दिया, जिसमें 2021 में 14 साल की किशोरी की मां का लड़की के निजी अंगों को छूने और पायजामे का नाड़ा तोड़ने का आरोप लगाया था। मामले में पॉस्को के अतिरिक्त बलात्कार व अपराध करने के प्रयास वाली धाराएं लगाईं गई थीं। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर नेटीजनों ने गहरी निराशा व्यक्त की थी तथा यह फैसला सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ था। 2021 में सबसे बड़ी अदालत ने नागपुर बेंच के बॉम्बे हाईकोर्ट के ऐसे ही फैसले को पलटते हुए कहा था, बच्चे के निजी अंगों को यौन इरादे से छूने को पॉस्को अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत यौन हिंसा माना जाएगा। नाबालिगों के साथ होने वाले यौन शोषण को लेकर पॉस्को सरीखे कानून बनने के बाद भी इस तरह के असंवेदनशील व स्त्रीविरोधी फैसलों का आना, बेहद विराचणीय है। यहां तक की सॉलीसिटर जरनल ने भी कहा कि इस फैसले पर मैं गंभीर आपत्ति जताता हूं। बलात्कार न भी हुआ हो तो किसी किशोरी को अंधेरी जगह में ले जाकर उसकी देह को नोंचना, छूना या उसके कपड़ों को उतारने के प्रयास को मामूली तो नहीं माना जा सकता। वहीं उक्त मामले के दो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जिन्हें आरोपियों ने तमंचा दिखाया। ऐसे में जब सारी दुनिया बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को महामारी से भयानक मान रही है, जिस पर सरकारों को गंभीरतापूर्वक काम करने की जरूरत है। सम्मानित अदालतों से बच्चों के अधिकारों की रक्षा की उम्मीद की जाती है। भाषा व शब्दों के चयन को लेकर इतनी संवेदना बनाये रखना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इसका असर दूर तलक जाता है।
Date: 28-03-25
कसौटी पर नेताओं की सहनशक्ति
रजनीश कपूर
हमारा देश विविधताओं का देश है, और इस विविधता में एक बात जो हर काल और हर कोने में समान रूप से पाई जाती है, वह है नेताओं पर व्यंग्य। चाहे वह गली-मोहल्ले की चाय की दुकान हो या सोशल मीडिया का चहचहाता मंच, नेताओं को लेकर हास्य और तंज का सिलसिला कभी थमता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे नेता इस व्यंग्य को सहन कर पाते हैं? या फिर यह हास्य उनके लिए एक कड़वी गोली बन जाता है, जिसे न निगलते बनता है और न उगलते? बीते दिनों एक और व्यंग्य को लेकर एक और विवाद हुआ जिससे यह विषय फिर से चर्चा में आ गया कि नेताओं और व्यंग्य का यह रिश्ता कितना गहरा और कितना नाजुक है।
नेताओं पर व्यंग्य कसना कोई नई कला नहीं है। प्राचीन काल से ही साहित्यकार, कवि और नाटककार शासकों और नेताओं की कमियों को उजागर करने के लिए हास्य रस का सहारा लेते आए हैं। भारत में चाणक्य से लेकर कबीर तक, और फिर आधुनिक युग में प्रेमचंद से लेकर हरिशंकर परसाई तक, व्यंग्य ने सत्ता को आईना दिखाने का काम किया है। परसाई जी ने तो अपनी रचनाओं में नेताओं की चालाकी, ढोंग और वादों की हवा को इस तरह उड़ाया कि पाठक हंसते-हंसते गंभीर सवालों पर ठिठक जाए। मसलन, उनकी एक कहानी में नेता चुनावी सभा में कहता है, ‘मैं आपके लिए जान दे दूंगा, और भीड़ तालियां बजाती है, लेकिन परसाई पूछते हैं, ‘क्या वह अपनी जान देगा या आपकी जान लेगा?’ आज के दौर में व्यंग्य का रूप बदल गया है। अब यह किताबों से निकलकर मीम, कार्टून और स्टैंड-अप कॉमेडी तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर हर दिन नेताओं के बयानों को तोड़-मरोड़ कर ऐसे चुटकुले बनते हैं कि आम आदमी हंसते-हंसते लोटपोट हो जाए। मगर इन चुटकुलों के पीछे एक कड़वा सच भी छिपा होता है। नेता जो जनता के सामने बड़े-बड़े वादे करते हैं, उनकी करनी और कथनी में काफी अंतर होता है। वहीं यदि नेताओं की सहनशक्ति की बात करें तो लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, और व्यंग्य भी अभिव्यक्ति का एक रूप है, लेकिन जब बात नेताओं पर तंज कसने की आती है, तो कई बार उनकी प्रतिक्रिया हैरान करने वाली होती है। कुछ नेता इसे हंसकर टाल देते हैं, तो कुछ इसे अपनी शान के खिलाफ मानकर कानूनी नोटिस भेजने से भी नहीं चूकते। वहीं कुछ नेताओं के कार्यकर्ता इस व्यंग्य को लेकर हिंसा करने में भी नहीं चूकते। उदाहरण देखाए – जब एक स्टैंड-अप कॉमेडियन ने किसी नेता के ‘विकास’ के दावों पर चुटकी ली। कॉमेडियन ने कहा, “नेता जी कहते हैं कि उन्होंने गांव में सड़क बनवाई, पर गांव वाले कहते हैं कि सड़क तो बन गई, बस गांव गायब हो गया !’ यह सुनकर दर्शक हंसे, लेकिन नेता जी ने इसे ‘चरित्र हनन’ करार देकर उस कॉमेडियन पर मुकदमा ठोक दिया। सवाल यह है कि क्या नेताओं को यह समझ नहीं कि जनता का हंसना उनके खिलाफ विद्रोह नहीं, बल्कि अपनी भड़ास निकालने का एक तरीका है? दूसरी ओर, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो व्यंग्य को खेल की भावना से लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसका बेहतरीन उदाहरण थे। उनकी कविताओं और हास्यबोध ने न केवल जनता का दिल जीता, बल्कि यह भी दिखाया कि एक नेता व्यंग्य को न सिर्फ सहन कर सकता है, बल्कि उसे अपने पक्ष में भी इस्तेमाल कर सकता है। एक बार संसद में उन पर तंज कसा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि सच सुनने की आदत जो पड़ गई है।’ एक स्वस्थ लोकतंत्र में व्यंग्य सिर्फ हंसाने का जरिया नहीं, बल्कि समाज का दर्पण भी है। यह नेताओं को याद दिलाता है कि वे अजेय नहीं हैं, और जनता उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है । जब नेता कोई अव्यावहारिक वादा करते हैं, जैसे ‘हर घर में सोने की चिड़िया लाएँगे, तो व्यंग्य के जरिए जनता पूछती है, ‘क्या चिड़िया अंडे भी देगी, या सिर्फ उड़ान ही भरेगी?’
यह हास्य सत्ता को जवाबदेह बनाए रखने का एक तरीका है, लेकिन व्यंग्य की यह ताकत तब कमजोर पड़ती है, जब उसे दबाने की कोशिश की जाती है। कई बार नेताओं के समर्थक या सरकारें व्यंग्यकारों को ‘राष्ट्रद्रोही’ तक करार दे देती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर है कि एक हंसी भी उसे हिला दे? नेताओं को यह समझना होगा कि व्यंग्य उनकी आलोचना नहीं, बल्कि उनकी लोकप्रियता का पैमाना है। नेताओं पर व्यंग्य और उसे सहन करने की क्षमता एक सिक्के के दो पहलू हैं । जहाँ व्यंग्य लोकतंत्र को जीवंत बनाता है, वहीं उसे सहन करने की कला नेताओं को जनता के करीब लाती है। यह न तो नेताओं को कमजोर करता है और न ही जनता को बेकाबू। यह बस एक संतुलन है, हंसी और गंभीरता का, सत्ता और जवाबदेही का । तो अगली बार जब कोई नेता मंच से बड़े-बड़े दावे करे, और जनता उस पर चुटकुला बनाए, तो दोनों को चाहिए कि इसे हंसकर टाल दें। आखिर, हंसी में जो ताकत है, वह गुस्से में कहां?
Date: 28-03-25
अभिव्यक्ति की आजादी से राजनीति
राज कुमार सिंह, ( वरिष्ठ पत्रकार )
विकसित भारत का लक्ष्य अभी दूर है, पर लगता है, देश भक्तिकाल से शक्तिकाल में पहुंच गया है। 15वीं शताब्दी के संत कवि कबीर दास ने लिखा था निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय | अब 21वीं शताब्दी में एक स्टैंड अप कॉमेडियन द्वारा किए गए व्यंग्य पर एक उप- मुख्यमंत्री की पार्टी उसे अपने ही ‘स्टाइल’ में देख लेने की धमकी दे रही है। ‘स्टाइल’ की झलक भी तोड़फोड़ के रूप में पेश की जा चुकी है। यह तब है, जब कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ‘आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है’।
बहरहाल, देश में तेजी से बढ़ते हास्य-व्यंग्य के बाजार में कुणाल कामरा नया नाम नहीं, पर एक ही विवाद से मिला दर्शकों व मददगारों का विशाल समूह किसी भी कॉमेडियन का सपना हो सकता है। 23 मार्च को यू ट्यूब पर अपलोड किए गए ‘नया भारत’ शीर्षक वाले उनके वीडियो को अब तक 34 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, तो देश-दुनिया से उन्हें समर्थन व आर्थिक मदद देनेवालों की संख्या भी बढ़ रही है। चंद दिनों में मिली इस लोकप्रियता के मूल में उनके वीडियो से भी ज्यादा निर्णायक भूमिका शायद उस पर महाराष्ट्र सरकार और उसमें शामिल एकनाथ शिंदे की शिव सेना की आक्रामक प्रतिक्रिया की है। कामरा ने कुछ मशहूर फिल्मी गानों की पैरोडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक पर तीखे कटाक्ष किए हैं। बेशक ये पैरोडी हास्य से ज्यादा राजनीतिक व्यंग्य हैं। कामरा को मात्र कॉमेडियन के रूप में नहीं, राजनीतिक व्यंग्यकार के रूप में देखना चाहिए। वह काफी समय से सीधे प्रधानमंत्री या केंद्रीय वित्त मंत्री को निशाना बनाते आए हैं, लेकिन वह निशाने पर तब आए हैं, जब उन्होंने एकनाथ शिंदे अर्थात शिवसैनिकों को निशाना बनाया है।
विडंबना यह है कि लड़ाई कानूनी प्रक्रिया से बाहर सड़क पर आ गई है। बीएमसी ने अचानक उस स्थल को तोड़ दिया, जहां कामरा ने वीडियो रिकॉर्ड किया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहते हुए कि कामरा को अपनी ‘निम्नस्तरीय’ कॉमेडी के लिए माफी मांगनी चाहिए, सरकार के सख्त रुख के संकेत दिए हैं, तो शिंदे की शिवसेना के कोटे से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कि अगर माफी नहीं मांगी, तो हम अपने स्टाइल में बताएंगे, वह कब तक छिपेगा । नागरिकों के जान- माल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सरकार के एक मंत्री की यह भाषा सवाल खड़े करती है। दूसरी ओर, कामरा का तर्क है कि उन्होंने तो शिंदे के बारे में वही कहा है, जो उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था।
बहरहाल, भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है। बेशक अनुच्छेद 19 के तहत दी गई। अभिव्यक्ति की आजादी पर 10 प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, पर वे देश की संप्रभुता, एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों से संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसावे से जुड़े हैं, न कि किसी सत्ताधीश के अहं से। फिर भी शिंदे और उनके समर्थकों को कामरा की पैरोडी की भाषा सीमा रेखा का उल्लंघन लगती है, तो कानूनी कार्रवाई का विकल्प उपलब्ध है। वैसे पैरोडी में शिंदे का नाम कहीं नहीं है।
विडंबना यह भी कि खुद को जिन बाला साहेब ठाकरे का ‘असली वारिस’ बताते हुए शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिव सेना तोड़ी, वह भी अपने तल्ख राजनीतिक कार्टूनों के लिए जाने जाते थे। हां, सच यह भी है कि कभी कार्टून के जरिये राजनीति और व्यवस्था पर तीखे कटाक्ष करनेवाले बाल ठाकरे की शिव सेना की अपने विरोधियों से निपटने की चिर परिचित ‘स्टाइल’ वही रही, जो शिंदे समर्थकों ने अपनाई है। दिलचस्प है कि उद्धव ठाकरे की शिव सेना खुल कर कामरा के बचाव में खड़ी हो गई है। इसलिए भी शिंदे को कामरा पर ‘सुपारी’ ले कर कॉमेडी करने का आरोप लगाने का मौका मिल गया है।
तात्कालिक विवाद से आगे देखें, तो कामरा शिंदे प्रकरण ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लक्ष्मण रेखा की शाश्वत बहस को फिर सतह पर ला दिया है। देश के बड़े कार्टूनिस्ट में शुमार आर के लक्ष्मण और केशव शंकर पिल्लई तथा उनके समकालीन राजनेता इसमें मार्गदर्शक हो सकते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के समकालीन शंकर तीखे राजनीतिक कार्टून के लिए जाने जाते थे । मित्रता के बावजूद नेहरू ने कहा था कि उन्हें भी न बख्शें। शंकर बख्शते भी नहीं थे, लेकिन उसका असर निजी रिश्तों पर कभी नहीं पड़ा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सीमा की बाबत आर के लक्ष्मण की यह टिप्पणी बेहद सटीक है: ‘व्यंग्य करते समय ‘गरिमापूर्ण अनादर’ होना चाहिए।’
अफसोस, मंच और यू ट्यूब पर जल्द लोकप्रियता की चाह में ज्यादातर कॉमेडियन ध्यान नहीं रखते कि शालीनता के दायरे में रहकर भी कटाक्ष किया जा सकता है। दूसरा पहलू यह भी है कि सत्ताधीश समाज और व्यवस्था में असहनशीलता तेजी से बढ़ रही है। ज्यादातर राजनेता और नौकरशाह, तनिक-सी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरे हर राज्य में देखे जाते हैं।
महाराष्ट्र में ही कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी का मामला अभी भी लोगों को याद है। साल 2012 में असीम को गिरफ्तार किया गया था, तब भी अभिव्यक्ति की आजादी पर खूब राजनीति हुई थी। वैसे, पश्चिम बंगाल में एक प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को तो अपनी सोसायटी के वाट्सऐप समूह में ममता बनर्जी संबंधी एक कार्टून को महज साझा करने की वजह से 2012 में गिरफ्तार कर लिया गया था। अंततः साल 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचकर ही प्रोफेसर को न्याय मिला। प्रोफेसर ने बरी होने के बाद पूछा था कि एक मामला खत्म हुआ, पर उन लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी, जिन्होंने मुझे पीटा था, मेरे साथ बहुत अभद्रता की थी?
यह कमी या परिपाटी पुरानी है। शासन-प्रशासन की खामियां उजागर करने का मीडिया से अपेक्षित दायित्व भी अनेक नेताओं को राष्ट्रविरोधी लगता है। नतीजतन, जनहित में आंख-कान बननेवाले खोजी पत्रकारों को भी कई बार प्रशंसा के बजाय कानूनी शिकंजा मिलता है। जनता को प्रजा और खुद को राजा समझने की यह मानसिकता जगह-जगह नजर आती है। ऐसे में, कम से कम राजनेताओं को संवेदना और एकरूपता का परिचय देना चाहिए, ताकि कम से कम अभिव्यक्ति की आजादी राजनीति का विषय न बनने पाए।