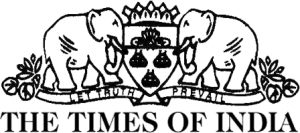25-11-2016 (Important News Clippings)
To Download Click Here
Unlock Lokpal Logjam
Centre must quickly complete all formalities and initiate appointment of Lokpal
The Supreme Court has rightly pulled up the Centre over its procrastination in appointment of a Lokpal despite the law being notified way back in January 2014. In this season of battling corruption and black money, an anti-corruption watchdog should be seen as vital. But appointment of one has been held up for two and a half years on what appears to be a merely technical matter.
The selection committee for appointing the Lokpal comprises the Prime Minister, Lok Sabha Speaker, Chief Justice of India or a sitting SC judge nominated by him, Leader of Opposition (LoP) and an eminent jurist nominated by the President to recommend names for the post of Lokpal. The technical hitch that has been raised is that there is no LoP currently. But this can be simply got around by amending the law to recognise the leader of the largest opposition party in Parliament as the LoP. If Parliament could amend other laws to expedite the appointments of CBI director, chief information commissioner and chief vigilance commissioner, then it can surely do so with respect to Lokpal.
Civil society leaders have also criticised the government for diluting the Lokpal Act by doing away with the statutory requirement of public servants to disclose assets of their spouses and dependent children. This goes against the spirit of transparency in public life where all judges of Supreme Court and High Courts and candidates contesting elections are required to disclose details of their assets and liabilities. The current NDA government was voted in with a decisive mandate after the previous UPA government was hit by a slew of corruption charges. It’s high time the government seized the initiative and gave the country a robust anti-graft watchdog.
Date: 25-11-16
Carrot and stick
Reintroduce the voluntary disclosure scheme to complement demonetisation
Into the third week of demonetisation a parallel economy in old currency notes has developed. Jan Dhan bank accounts have seen an extraordinary flow of Rs 21,000 crore in deposits. Old currency is being flown to Nagaland, presumably to take advantage of loopholes, and drivers transporting cash are disappearing with their consignment. It appears as if all of India’s productive energies are now deployed to either legitimately withdraw cash or find ways to beat the system. For the government, it is time to change tactics now.
Demonetisation is a punitive measure and has signalled the Narendra Modi government’s resolve to combat black money. However, punitive measure have limitations as the last few days have shown. Even authoritarian regimes using draconian methods have been unable to stamp out black markets. The best way forward would be to combine punitive measures with incentives to encourage people to disclose unaccounted income and assets. Having signalled its resolve, the Modi government should now introduce an incentive that will mitigate economic disruption and earn it additional revenue.
The Income Declaration Scheme 2016 – which allowed people to pay 45% tax, surcharge and penalty in three installments for hitherto undisclosed income – should now be reintroduced for a couple of months. A combination of carrot and stick works best to incentivise disclosures of unaccounted money. The gains would go to the government in the form of tax revenue and a widening of tax base. In the absence of an incentive, what we will see is a wealth transfer within the firmament of illegal activities as black money gets recycled, not extinguished. This, in turn, will be followed by the return of an enforcement state, which will not be more successful than the one which existed in the 1970s.
India’s fight against black money has been dominated by punitive measures as it sends political signals. But this is primarily an economic problem which needs to be tackled through economic tools. Economic policies such as rollout of GST, which will provide traders and manufacturers an incentive to disclose transactions, are integral to dealing with the problem. In addition, a move to trim tax rates and simultaneously close down loopholes will make tax evasion an unattractive proposition. While policy changes are long term remedies, the immediate need is an income disclosure scheme to complement punitive measures.
तलाशें समाधान
न्यायिक नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच लंबे समय से चली आ रही लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह दोनों पक्षों की साझा जिम्मेदारी है कि वे एक स्वीकार्य हल तलाशें, जिसमें न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही की जरूरत जैसे दोनों हित सुनिश्चित हो जाएं। हाल के दौर में असहमतियां बढ़ी हैं। इस महीने की शुरुआत में केंद्र ने उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए 43 नामों को खारिज कर दिया था। फिलहाल इन न्यायालयों में कॉलेजियम के माध्यम से ही नियुक्ति होती है।
उच्चतम न्यायालय ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर वाले दो सदस्यीय पीठ ने कहा, ‘उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए हमने उन 43 नामों को ही दोहराया है, जिन्हें सरकार ने खारिज कर दिया और उन्हें पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया है।’ यह भी सच है कि जब तक नई व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ जाती, तब तक सरकार को उन नामों पर मुहर ही लगानी होगी, जो उसके पास पुनर्विचार के लिए आएंगे।
न्यायमूर्ति ठाकुर अगले वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वह हमेशा न्यायिक स्वतंत्रता के बड़े हिमायती रहे हैं। पिछले महीने उनके एक पीठ ने ने महान्यायवादी मुकुल रोहतगी की मौजूदगी में सरकार से कहा था कि वह न्यायपालिका पर बंदिशें लगाने पर आमादा है। शीर्ष अदालत के इस आरोप पर सरकार ने तल्खी से जवाब दिया। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दलील दी कि सरकार ने इस साल उच्च न्यायपालिका में 120 नियुक्तियां की हैं और कहा है कि यह आंकड़ा एक साल में सबसे ज्यादा नियुक्तियों के रिकॉर्ड से महज एक कम है। हालांकि इससे पूरी कहानी स्पष्टï नहीं होती। तथ्य यही है कि मई, 2015 से उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की निर्धारित संख्या और इन पदों पर काबिज न्यायाधीशों की संख्या में अंतर तकरीबन 7 फीसदी से बढ़कर लगभग 43 फीसदी तक पहुंच गया। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने पर भी सहमत हो गई लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं था। मौजूदा दौर में नियुक्ति प्रक्रिया पर हो रही बहस दो सवालों की ओर मुखातिब हो जाती है, जो प्रस्तावित प्रक्रिया से जुड़े हैं, जो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार तैयार करेगी। पहला सवाल तो यही है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति को खारिज करने की मंशा जताई है। दूसरा यही है कि कॉलेजियम द्वारा किसी भी न्यायाधीश को प्रोन्नत करना या हटाने का कारण देना होगा। इन असहमतियों में सही भाव प्रभावी होना चाहिए और दोनों पक्षों के कुछ न कुछ आग्रहों पर ध्यान दिया जाए। मिसाल के तौर पर अदालतों के लिए यह मानना बेहतर होगा कि अपनी पसंद के लिए वे ज्यादा पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करेंगी। इससे दीर्घ अवधि में न्यायपालिका में भरोसा और मजबूत ही होगा। इस बीच सरकार को भी निश्चित रूप से समझना चाहिए कि ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ बेजा इस्तेमाल होने वाला जुमला है। इसके दुरुपयोग की आशंका है।
अगर कॉलेजियम व्यवस्था कायम रहे और सरकार किसी विशेष न्यायाधीश को लेकर चिंतित हो तो वह उन चिंताओं को कॉलेजियम के साथ साझा कर उसे विश्वास में ले और उसके निर्णय का सम्मान करे। कार्यपालिका के पास व्यापक और खुली वीटो शक्ति भी ठीक नहीं होगी और इससे न्यायिक स्वतंत्रता बाधित होगी। इस समस्या का समाधान पहुंच में हैं। इसे और अधिक टालना नहीं चाहिए।
कमजोर रुपया : गिरती कीमत के तीन बड़े असर

मजबूत डॉलर
Rs.70
प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच सकता है रुपया आने वाले कुछ महीनों में।
 तेल कंपनियों की तरफ से डॉलर की डिमांड बढ़ी है।
 विमुद्रीकरण के चलते भी रुपए पर असर देखा गया।
 डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने भी डॉलर को मजबूत करने की दिशा में सहारा दिया है।
खुशहाल होने के लिए जरूरी है कुपोषण से लड़ाई

ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जहां कुपोषण अपवाद नहीं, आम बात है। देश भर में पांच वर्ष की आयु से पहले ही हर वर्ष मरते 13 लाख बच्चों में से करीब आधे की मौत का कारण कुपोषण है। इसके शिकंजे से जीवित बच जाने वाले बच्चों को भी उसका दुष्परिणाम जीवन भर झेलना पड़ता है। सही भोजन न मिलने से उनके दिमाग और शरीर हमेशा के लिए कमजोर हो जाते हैं। भारत में पांच वर्ष से छोटे करीब 4.4 करोड़ बच्चे ठिगने हैं। यानी उनका विकास सामान्य गति से नहीं हो पाया। इस कारण उन्हें पढ़ने में और बाद में आजीविका कमाने में दूसरों से अधिक कठिनाई होती है।
स्वस्थ बच्चों की तुलना में कुपोषित बच्चों में आजीवन कमाई की क्षमता एक-चौथाई कम होती है। एक अध्ययन के अनुसार कमाई में इस क्षति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 46 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेडिकल स्कूल में मुझे सिखाया गया था कि कुपोषण को स्वास्थ्य की समस्या माना जाए। लेकिन गेट्स फाउंडेशन के मेरे रोज के काम से यह सिद्ध हो जाता है कि कुपोषण एक आर्थिक समस्या भी है। हम अपने बच्चों को जो कुछ खिलाते हैं, उसका हमारी अर्थव्यवस्था की शक्ति से गहरा संबंध है। जब कोई देश कुपोषण पर जीत हासिल कर लेता है तो उसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रति वर्ष 2-3 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।
अच्छी बात यह है कि कुपोषण का सामना करने के लिए आज हमारे पास पहले से अधिक जानकारी और साधन मौजूद हैं। बच्चे चाहे कहीं रहते हों और उनकी परिस्थितियां कैसी भी हों, उनकी समस्याओं से निपटने के लिए जांचे-परखे समाधान उपलब्ध हैं। इनमें प्रसव के तुरंत बाद माताओं को अपने शिशुओं को स्तनपान कराना और छह महीने का होने पर बच्चे को पोषक और सुरक्षित आहार देना शामिल है। स्तनपान कराने से न सिर्फ बच्चे का जीवन बचता है, बल्कि अध्ययन बताते हैं कि स्तनपान करने वाले बच्चे स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पोषाहार संबंधी कदम समस्या का आंशिक समाधान ही कर पाते हैं। वे सबसे अधिक असरदार तभी होते हैं, जब लड़कियों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था हो, उनकी सही समय पर शादी और गर्भधारण हो। फिर सुरक्षित पेयजल सुलभ कराया जाए, व्यापक स्तर पर टीकाकरण किया जाए और खेती से वर्ष भर सुरक्षित, कम खर्चीला और पौष्टिक आहार सुनिश्चित किया जाए। यह सब इतना आसान नहीं है। फिर भी हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए।
कई मुल्कों ने इन मामलों में तेजी से प्रगति की है। उन्होंने कुपोषण उन्मूलन को राष्ट्रीय अजेंडा बनाया। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल कायम किया है। उन्होंने अपनी जवाबदेही निश्चित करने के लिए कुछ सिस्टम विकसित किए। जैसे, ब्राजील में कुपोषण पूरी तरह समाप्त हो गया है और एक पीढ़ी में 80 प्रतिशत लोगों के लिए वृद्धि और विकास के अवरोध कम होने लगे हैं। मैंने इस महीने जो कुछ देखा और सुना है, उसके आधार पर भारत के लिए आशावान होने के कई कारण हैं। भारत, नमक में आयोडीन मिलाने, विटामिन ए की पूरक खुराक देने और साल में दो बार कीड़े निकालने की दवा देने, स्तनपान सुधारने और बड़े पैमाने पर आहार को पुष्ट करने के संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। अपनी इस यात्रा के दौरान महिला और बाल विकास मंत्रालय के लोगों से मेरी मुलाकात सबसे बेहतर रही। यह जानकर बेहद खुशी हुई कि मंत्रालय सामाजिक और आचरण परिवर्तन संबंधी संदेशों की क्षमता का उपयोग करेगा, अधिक कारगर संवाद और रिपोर्टिंग के लिए बेहतर टेक्नॉलजी अपनाएगा और बेहतर पोषण को बेहतर स्वच्छता से जोड़ेगा।
(लेखिका बिल ऐंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सीईओ हैं)
Date: 25-11-16
नई विश्व राजनीति की आहट
जो लोग डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारतीय चलन से यह कह रहे थे कि ट्रंप ने कई बातें केवल चुनाव जीतने और लोगों को बरगलाने के लिए की थीं उन्हें पश्चिमी नैतिकता का सही अंदाजा नहीं है। उनका अनुमान ट्रंप ने फौरन ध्वस्त कर दिया। रिटायर्ड जनरल माइकल फ्लिन्न को अमेरिका का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मनोनीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह ‘रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म’ को खत्म करने में मदद करेंगे। यह अमेरिकी और साथ-साथ विश्व राजनीति की शब्दावली में बहुत बड़े परिवर्तन की घोषणा है। एक अर्थ में इस्लामी विश्व से संबंधित अनेक समस्याओं के प्रति अब तक के चलन को यह एक झटके में तोड़ने वाला कदम है। अब तक सभी औपचारिक बयानों में इस्लाम के प्रति केवल सकारात्मक विशेषण लगाने का चलन था। ट्रंप ने इसे खत्म कर बेलाग बात कहने की नई परंपरा शुरू की है। यूरोप भी इसी दिशा में बढ़ रहा है। रूस और ब्रिटेन के बाद इसकी झलक फ्रांस से भी मिल रही है। वस्तुत: समस्याओं को बेलाग रखने से ही चुनाव अभियान में ट्रंप को ख्याति और कुख्याति मिली थी। चूंकि अमेरिकी जनमत ने उन्हें ही चुना इसलिए अब उस नजरिये पर नैतिक और कानूनी मुहर भी लग गई है। ट्रंप द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, रणनीतिक पदों पर साफ विचारों वाले लोगों की नियुक्ति का अर्थ है कि उन विचारों के अनुरूप ही नीतियां बनेंगी और लागू होंगी। भारत के लिए यह बड़ा अवसर है।
माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख रखेगा। पिछले 15 वर्षों के अंतहीन अनुभवों से अब तक सैकड़ों अमेरिकी नीतिकारों, सीनेटरों, कमांडरों, पत्रकारों को भी अच्छी तरह मालूम है कि ‘आंतकवाद से लड़ने’ के नाम पर पाकिस्तान ने बेशर्मी से दोहरा खेल खेला है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, कश्मीर और स्वयं अपने यहां आतंकियों को नियंत्रित रूप से पालने-पोषने का काम किया है, ताकि अमेरिकी, यूरोपीय धन, हथियार और यथासंभव कूटनीतिक सहयोग सदा मिलता रहे। इसके लिए अमेरिकी हथियारों से खुद अमेरिकियों को भी मारा और वह भी जानबूझकर। हाल की चर्चित पुस्तक ‘फयेरवेल काबुल’ में इसके अनगिनत प्रमाण हैं। यह सब इसलिए ताकि अफगानिस्तान में आतंकवाद खत्म न हो। अन्यथा पाकिस्तान को पश्चिम से मिलने वाली धन की वह नहर सूख जाएगी, जिससे भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध और पाकिस्तानी जनरलों, नेताओं की अपनी-अपनी जेबें भरना भी चलता रहा है। ट्रंप प्रशासन इसे बंद करेगा या अत्यधिक कम करेगा। इससे पाक का एक मूल शक्ति-स्रोत इतना क्षीण हो जाएगा जिसके परिणामों की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में भारत यदि इस्लाम के नाम पर जारी आतंकवाद के प्रति अपनी झिझक छोड़ विश्वास के साथ, संयत और सुलझे रूप में इसके हर रूप के विरुद्ध कुछ न कुछ छोटा भी, लेकिन ठोस कार्य करे तो बड़ा लाभ होगा। वस्तुत: पाकिस्तान समस्या के साथ-साथ देश के अंदर कथित सांप्रदायिक समस्या का भी स्थाई हल होना आरंभ हो सकता है।
अब तक भारत की झिझक नेताओं, बुद्धिजीवियों के अज्ञान के अलावा ‘विश्व राजनीति की नाजुक’ और ‘मुस्लिम संवेदना’ के कारण भी रही है। अरब देशों की नाराजगी और देश के मुस्लिम नेताओं के भय से हमारी सरकारें बहुतेरी गलत काम करती रही हैं। इसमें सबसे प्रमुख है मजहब के नाम पर किए जाने वाले जोर-जुल्म की अनदेखी करना और संविधान एवं कानून को भी मुस्लिम नेताओं की जिद के अधीन कर देना। कश्मीर से हिंदुओं के सफाये या तसलीमा नसरीन पर इस्लामी नेताओं की हिंसक कार्रवाइयों, बयानबाजियों पर हैदराबाद से लेकर कोलकाता और दिल्ली तक चुप्पी रखना इसके उदाहरण हैं। यह सब सदा के लिए समाप्त होने का अवसर खुल रहा है। ध्यान दें स्वयं मुस्लिम समाज के बीच सुधार करने या इस्लामी कायदों की जकड़ खत्म करने की मांग तेज हो रही है। 28 वर्ष पहले सलमान रुश्दी को मार डालने का विश्वव्यापी अभियान चला था। आज उससे दस गुनी आलोचनात्मक बातें कहने वाले मुस्लिम विचारक और एक्टिविस्ट कई देशों में सक्रिय हैं। इस बदलाव का महत्व समझकर सुधारवादी मुस्लिमों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। अब यह खुलकर, लेकिन सद्भावपूर्वक कहने की जरूरत है कि इस्लाम के नाम पर आतंकवाद सबसे अधिक मुसलमानों को तबाह कर रहा है। पाक, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से भारतीय जनजीवन की तुलना से इसे साफ समझा जा सकता है। अधिक देखने के लिए सीरिया, इराक, सऊदी अरब आदि की स्थिति भी देखी, दिखाई जानी चाहिए।मुस्लिम समुदाय की सारी समस्याओं के लिए अमेरिका, इजराइल या भारत को दोषी ठहराने का समय खत्म हो चुका। उनकी समस्याओं की जड़ उनकी मध्युगीन विचारधारा, शरीयत और उलमा की जकड़ आदि में है। भारत के नेताओं, पत्रकारों, समाजसेवियों को विश्वास के साथ मुसलमानों को उनसे मुक्त होने के लिए आग्रह करना चाहिए। चूंकि सेक्युलरिज्म सबके लिए है अत: इस्लामी राजनीति, इस्लामी कानून को बीते समय की चीज मानकर मुसलमानों को भी नजरिया बदलने का निमंत्रण देना चाहिए। स्वयं मुसलमान इसे धीरे-धीरे स्वीकार कर रहे हैं। इसका उदाहरण मुस्लिम देशों व उलमा की प्रतिक्रिया में बदलाव है।जिस तरह, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में दुनिया के मुस्लिम समुदाय को कठघरे में खड़ा किया और अब माइकल फ्लिन्न को नियुक्त करते हुए ‘इस्लामी आतंकवाद’ को खत्म करने का लक्ष्य रखा उस पर अरब या एशिया के मुस्लिम समुदायों में कोई उग्र बयानबाजी नहीं हो रही है। पहले ब्रेक्जिट और अब ट्रंप की जीत का मतलब यही है। यूरोप और अमेरिका की जनता अब मान चुकी है कि मीठी बातें करके, विविध इस्लामी मांगों के आगे झुककर मुस्लिम नेताओं से कोई शांति या सहयोग नहीं मिला। अब वे साफ-साफ बातें करने का मन बना चुके हैं। ट्रंप को मिली जीत इसकी स्वीकृति है कि मुस्लिम नेताओं से बराबरी, लोकतंत्र और यथार्थपरक बातें की जानी चाहिए। अन्य धर्मों और उनकी मान्यताओं को उपेक्षित कर केवल इस्लाम को तरजीह देने का काम अब नहीं चलेगा। यही चीज भारत में और सरलता से मुस्लिम समाज से कही जा सकती है और कही जानी चाहिए। चूंकि भारत में सभी धर्मों के प्रति सहज आदर रखने वाले मुस्लिम सबसे बड़ी संख्या में हैं इसलिए यहां वास्तविक समानता को लागू करना अधिक आसान है। मुट्ठी-भर इस्लामी कट्टरपंथियों ने वोट-बैंक का लोभ और हिंसा का भय दिखा-दिखा कर दलों को ब्लैकमेल किया है। यह लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म और समानता, तीनों के विरुद्ध है। यदि भारत के लोग बदलते युग का संकेत समझ कर अपनी नीतियों में सही बदलाव ला सकें तो बहुत बड़े वैश्विक परिवर्तन के भागी हो सकते हैं। इससे पूरी मानवता और भारत की होने वाली भलाई का अभी अनुमान भी नहीं किया जा सकता।
[ लेखक शंकर शरण, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं ]
Streamline the appointments
The judiciary must give up its reluctance to accept performance indicators and impart transparency to the collegium process.

That takes us to the collegium system, in existence since the Second Judges Case of 1993 and validated by the Special Reference of 1998, though the Constitution mentions no such collegium. Strictly speaking, there are two levels of the collegium — high court and Supreme Court. Recently, a judge of the SC said, “I have written a letter informing him (CJI) that I will not be participating in the collegium’s meetings henceforth. The system of selection of judges is not at all transparent. No reason, no opinion is recorded. Just two people decide the names and come back to the meeting and ask for a yes or no. Can a judge of the SC or HC be selected in such a manner?” If Justice Chelameswar is forced to say this, the statement cannot be taken lightly. It therefore follows that the collegium system needs to become more transparent, especially in an environment where there is a drive towards transparency all around and courts have themselves urged the rest of society to move towards transparency. Consider this: What percentage of names recommended by different HC collegiums are rejected by the SC? Figures of between 30-35 per cent float around. Since no one is seeking information about specific individual names, why can’t that aggregate information be published in Court News? .
When does the collegium process, at either level, kick in? Unless it is truly Manus Dei, one knows in advance when there will be permanent vacancies. Does the collegium process kick in six months in advance? If there are a certain number of vacancies, does the HC collegium recommend exactly that number, or some multiple of it? On what basis are selections made? “This legitimate expectation has relevance on the ground of longer experience on the Bench, and is a factor material for determining the suitability of the appointee, Along with other factors, such as, proper representation of all sections of the people from all parts of the country, legitimate expectation of the suitable and equally meritorious judges to be considered in their turn is a relevant factor for due consideration while making the choice of the most suitable and meritorious amongst them, the outweighing consideration being merit, to select the best available for the apex court.” This is from the 1993 judgement, quoted in 1998. Ipso facto, everything cannot be on the basis of seniority and there must be some attempt to gauge “merit”, not just from within the judiciary, but also from outside, such as the bar.
Any selection process has a similar set of principles. True, everything cannot be reduced to a GPA. But that doesn’t mean everything must be left vague, indeterminate, subjective and non-transparent. In any organisation, the higher the position, the more difficult it is to quantify performance. However, performance-based indicators aren’t impossible, even if those don’t become the sole determinant. Recently, the Vidhi Centre for Legal Policy has developed such a judicial performance evaluation system for judges of the SC and high courts. I have no intention of suggesting that this is perfect. That perfection and tweaking should be done by insiders — judges themselves.
Vidhi, or something like that, is no more than a suggested template. In the entire controversy over NJAC, I cannot fathom the judiciary’s reluctance to accept performance indicators and impart transparency to the collegium process. While protecting the independence of the judiciary, nor do I understand the reluctance to accept the help of a screening committee, especially in a situation where time, for a heavily-burdened judiciary, is at a premium. In several other instances, screening committees routinely exist as filters. They facilitate the work of selection committees and no more. The proposed Memorandum of Procedure (MOP) seems to be stuck now. I am reminded of something Benjamin Franklin wrote in Poor Richard’s Almanack: “There are three things extremely hard, steel, a diamond, and to know one’s self.” If the SC did the last, I think the steel of confrontation would disappear and a diamond would result.
Date: 24-11-16
Partial cure
E-pharmacy guidelines for self-regulation is welcome. But more is needed to regulate chemists and pharmacies

The Drugs and Cosmetics Act, 1940, requires a retailer to check a licensed and registered doctor’s prescription in the presence of a pharmacist. But it is common knowledge that a vast majority of retailers in the country do not meet this requirement. Prescription drug abuse — using dated prescriptions or using medicines legally bought by a person who no longer needs them — is also rampant. There are, however, no credible figures that convey the exact magnitude of the problem. The last survey undertaken 15 years ago, was a part of a broader survey on drug and narcotic abuse in the country, and it did not provide any figures. A more comprehensive survey could be a good first step to track the extent of prescription drug abuse in India.
E-pharmacies present a different order of problem. There are less than 15 such pharmacies in the country today. However, this segment is poised to expand. Industry estimates reckon that $18 billion e-pharma market is expected to grow three times by 2020. The Drug and Cosmetics Act, 1940, is obviously not equipped to deal with this business. The guidelines issued recently are a good first step. But there should be mechanisms that allow proper tracking and monitoring of sales of drugs, check the authenticity of online pharmacists and scrutinise prescriptions and details of patients. Proper care should also be taken to ensure patients’ privacy. Online portals can aggregate supplies, making otherwise-hard-to-find medicines available to consumers across the country. But they need to be regulated well.
Where are our legal philosophers?
We need them to help us frame pertinent questions about judgments and the framework for a law-abiding society
In recent times, when our most fundamental understanding of concepts of law and its interplay with perceptions of justice, morality, humanism, freedom, honour and virtue are being questioned with fierce candour in the media and every conceivable public space, legal philosophy is all we have to guide our path. Sadly, a country that once based its laws on the commentaries of legal philosophers has allowed that tribe to become almost extinct.
In a society that seeks to rest its foundations in justice, a legal philosopher performs three essential functions. First, he expounds the relationship between law, justice and other concepts so fundamental to explain the nature of human existence in society. Second, he critically examines existing legal philosophies. Third, he examines decisions of courts and legislations from the point of philosophic principles.
Propounding legal principles
Through the centuries, many legal philosophers left their indelible mark on shaping institutions of governance. Many of the systems of governance and rule of law as are familiar today have been developed by applying principles expounded by legal philosophers. To Aristotle, justice was all about “giving every person his due” and the purpose of law was to develop a just society that made this possible. Kautilya’s Arthashastra postulated that the king was the fountainhead of justice but with the limitation that even he was obliged to rule according to the Dharmashastras. William Blackstone, through his book, Commentaries on the Laws of England, guided the growth and development of English law in no small measure; John Austin popularised the theory that law was command of the sovereign made credible by threats of punishment for its disobedience. The horrors of the World Wars galvanised dialogue on a new wave of legal philosophy that recognised the existence of some inalienable rights in every individual that could not be eliminated even by state-made laws. One could also discern their application in the famous Nuremberg trials where the defence of the Nazi officers — that they could not be punished because everything they did was in execution of valid legal commands — found no acceptance. The path-breaking work of several legal philosophers of that time had their impact in the promulgation of certain important international documents and treaties like the Charter of the United Nations, Universal Declaration of Human Rights, European Convention on Human Rights and the 1959 Declaration of Delhi on the rule of law.
This leads us to perceive the second function of a legal philosopher, to examine the validity of claims put forth by other legal philosophers. Take the theories of Lon Fuller in The Morality of Law. In this work Fuller creates a fictional King Rex who fails in the exercise of his lawmaking powers because (a) the laws do not have universal application, with the result that every case gets decided on an ad hoc basis; (b) his subjects remain ignorant of the rules he makes; (c) his law-making is an abuse of authority as he constantly keeps making retrospective legislation; (d) his rules suffer from lack of clarity; (e) his rules contradict each other; (f) his rules are subject to such frequent changes with the result that they give little time for subjects to adjust their actions; (g) he fails to ensure that the rules as administered are rules that have been enacted. Fuller claimed that a just king in his administration of justice avoids completely the debacles of King Rex’s system. Initially applauded, latter-day critics dissented from his views, pointing at apartheid rule in South Africa which was, applying Fuller’s prescriptions, undoubtedly effective but still far from being just.
Legal philosophy and court verdicts
The third function of a legal philosopher is to examine closely judicial pronouncements and legislations from philosophical perspectives. For instance, in India, a legal philosopher would have possibly raised the following questions about the National Judicial Appointments Commission judgment: If the Constitution of India is the social contract between the state and the citizen, through which provision of this social contract has the citizen vested “primacy” in the judiciary to select judges? If the source is not to be found in the written Constitution but in the “basic structure” doctrine, then is that doctrine a supplementary social contract that can be traced to a source other than the will of the people? If so, what is this source and what are its contours? Can Parliament bring in a legislation exhaustively declaring the “basic structure” on the plea that it needs guidance to its legislative exercise? Would that legislation itself be likely to be struck down as offending the principle of “basic structure”?
Or take the recent decision of the Supreme Court which holds that a wife demanding that her husband be separated from his parents is a ground for divorce. A legal philosopher would ask: Can this observation of the court be treated as a general norm? Is a wife to be treated as a means by the husband and/or his family to achieve their “cultural aspirations”, or is she to be recognised as an individual deserving mutual respect and dignity? A legal philosopher may even expand the scope of his inquiry to ask, is any human being entitled to treat another human being, or even our sentient fellow creatures and environment, as merely a means to their happiness and well-being, or is the dignity and mutual respect of the entities we interact with to be the prime focus of a just and law-abiding society? The questions are perplexing and a quest to find answers can be daunting… but where are our legal philosophers to question and to seek?
N.L. Rajah is a senior advocate of the Madras High Court.
खात्मे की तरफ मनरेगा!
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अर्थात मनरेगा के तहत बकाया मजदूरी का सवाल अब सुर्खियां बनता दिख रहा है। पिछले दिनों सीतापुर, उत्तर प्रदेश से आई खबर आंखें खोलनेवाली है, जिसके मुताबिक अकेले सीतापुर में भारत सरकार को अभी तीस करोड़ रुपये देने है। ताकि बीते पांच महीने में लोगों ने जो काम किया है, उसका भुगतान हो सके। जाहिर है इस बकाये के भुगतान के लिए इलाके के मजदूर किसानों ने जिला मजिस्टेट तथा विकास अधिकारी के कार्यालयों पर धरने-प्रदर्शन किए हैं, मगर उनकी आवाज अनसुनी कर दी गई है। और यह अकेले सीतापुर का मामला नहीं है। अब खबर आ रही हैं कि ग्रामीण गरीबों के जीवन में, हाशियाग्रस्त समुदायों की स्थिति में थोड़ी बेहतरी लाने में सफल इस योजना को लेकर केन्द्र सरकार ने अनआफिशियल स्तर पर फंड में कटौती का दायरा देशव्यापी बना दिया है।गौरतलब है कि इस अकाल वर्ष में, जबकि ग्रामीण इलाकों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत काम की मांग बढ़ी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक ‘‘व्हाटसएप चाट ग्रुप’ का इस्तेमाल राज्यों को यह बताने के लिए किया कि वह इस अहम योजना के नाम पर गरीबों के लिए अधिक काम निर्माण करने से बचें। अगस्त में भेजे अपने इस संदेश में राज्य सरकार के अधिकारियों को बताया गया कि मनरेगा के तहत रोजगार निर्माण की ‘‘अंधी दौड़’ जारी नहीं रह सकती। केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने अधिकारियों को यह चेतावनी भी दी कि इसके लिए अधिक फंड उपलब्ध नहीं किए जाएंगे और राज्य सरकारों को इस मद में जितनी धनराशि पहले से मिली है, उसे ही उन्हें अधिक ‘‘संतुलित’ ढंग से इस्तेमाल करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल केन्द्र सरकार साल की शुरुआत में लेबर बजट तैयार करती है- जिसमें इस बात का एक स्थूल अनुमान होता है कि आगामी वित्तीय वर्ष में वह कितने दिनों का काम कितने व्यक्तियों के लिए निर्माण करेगी। इसे राज्यों के साथ सलाह-मशविरा करके तय किया जाता है, अलबत्ता केन्द्र सरकार को इसमें अंतिम निर्णय लेना होता है। इस साल केन्द्र सरकार ने 217 करोड़ व्यक्ति दिनों के काम के निर्माण की बात की थी- जो राज्यों द्वारा सलाह दिए गए दिनों से 98 करोड़ मानव दिवस कम था। और उसने राज्यों को यह निर्देश भी दिया था कि उसके द्वारा तय इस सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अनौपचारिक स्तर पर लगाए गए इस प्रतिबंध को लेकर कई सारे राज्यों ने केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय के साथ बात करने की कोशिश की और उस पर यह जोर डाला कि वह पहले से बकाया सैकड़ों करोड़ रुपयों की राशि को तत्काल जारी कर दे, मगर इस बात को देखते हुए कि केन्द्र सरकार ने ऑफ द रेकार्ड निर्देश जारी किए हैं, विभिन्न राज्यों द्वारा इसी योजना के तहत दिए जा रहे काम में अगस्त एवं सितम्बर माह में जबरदस्त गिरावट देखी गयी। मौजूदा सरकार ने इस योजना को लेकर अपने आधिकारिक रुख को लेकर तब यू टर्न लिया जब इस योजना को दस साल पूरे हुए, मगर जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं बदला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फूड कमीशनर के दफ्तर के लिए प्रमुख सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए बिराज पटनायक का साक्षात्कार इस मामले में आंखें खोलनेवाला रहा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि आला अदालत द्वारा इस मामले में स्पष्ट तथा सख्त निर्देश के बावजूद सूखाग्रस्त इलाकों में जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं चला था। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने इस साल इस योजना के लिए 43,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, मगर वह इस सच्चाई को छिपाता है कि उसमें से 12,000 करोड़ रुपये पिछले साल की मनरेगा मजदूरी का बकाया ही था। और सूखे के इस वर्ष में त्रासदी यह है कि बीते सालों की तुलना में 220 मिलियन मनरेगा दिनों का आवंटन घटा दिया गया है। जहां गरीबों के लिए, भुखमरी की कगार पर खड़े लोगों के लिए खजाने के दरवाजे खोलने में सरकार सकुचाती दिखती है, वहीं दूसरी तरफ इस सरकार को कोई ग़म नहीं कि वह बैड डेब्टस अर्थात खराब कज्रें के नाम पर इस देश के पूंजीपतियों द्वारा सरकारी बैंकों से लिया गया लाखों करोड़ रुपयों का कर्जा माफ कर दे, भले ही उससे सरकारी बैंकों का दीवाला पीटने की नौबत आए, भले ही वहां जमा पैसे का अधिकतर हिस्सा आम लोगों की गाढ़ी कमाई से आता हो।
सुभाष गाताडे