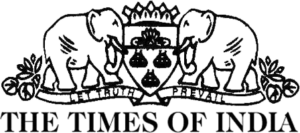18-05-2016 (Important News Clippings)
To Download Click here.
निवेश दर में सुधार से वृद्घि को मिलेगी धार
अगर देश में 8 से 9 फीसदी की जीडीपी दर सुनिश्चित करनी है तो 30 प्रतिशत से नीचे जा चुकी निवेश दर को दोबारा 35 प्रतिशत से ऊपर लाना होगा। बता रहे हैं अजय छिब्बर
दीर्घावधि की वृद्घि में सुधार काफी हद तक निजी निवेश में सुधार पर निर्भर करता है। वर्ष 2003-2004 से 2007-2008 के दौरान हुई तेज वृद्घि जिसे जीडीपी वृद्घि का स्वर्णकाल कहा जाता है वह निजी निवेश में हुई बढ़ोतरी पर ही आधारित थी। वैश्विक संकट के बाद जब निजी निवेश में तेज गिरावट आई, तो वृद्घि तो बरकरार रही लेकिन उसे गैर कारोबारी निजी निवेश ने गति दी। खासतौर पर सेवा क्षेत्र, अचल संपत्ति और राजकोषीय प्रोत्साहन ने। लेकिन उसे निरंतरता नहीं प्रदान की जा सकी।
निजी निवेश को सुधारने के लिए क्या आवश्यक है? नया दिवालिया कानून एक स्वागतयोग्य पहल है लेकिन इसका क्रियान्वयन वक्त लेगा। कारोबारी सुगमता में सुधार लंबी अवधि में मददगार होगा। लेकिन अन्य तात्कालिक नीतिगत कदमों का प्रयोग भी निजी निवेश बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। पुराने जीडीपी आंकड़ों यानी 1980 से 2013-14 के आंकड़ों पर किया गया विश्लेषण बताता है कि वास्तविक विनिमय दर, निजी क्षेत्र को ऋण और सार्वजनिक बुनियादी निवेश, इन्हीं तीनों क्षेत्रों में 90 प्रतिशत निजी निवेश हुआ। परंतु कॉर्पोरेट और गैर कॉर्पोरेट निवेश पर इसका बहुत अलग प्रभाव रहा।
सार्वजनिक बुनियादी निवेश में निजी निवेश की भरमार है। सार्वजनिक बुनियादी निवेश में हर प्रतिशत की बढ़ोतरी पर निजी निवेश 1.1 प्रतिशत बढ़ा। इसका गैर कॉर्पोरेट निवेश पर बड़ा प्रभाव है क्योंकि सार्वजनिक बुनियादी क्षेत्र के हर प्रतिशत इजाफे पर इसमें 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कारोबारी निवेश पर भी सार्वजनिक बुनियादी क्षेत्र का सकारात्मक प्रभाव पड़ा लेकिन उतना नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कारोबारी निवेश व्यापक है।
वास्तविक विनिमय दर का निजी निवेश पर व्यापक असर होता है। वास्तविक विनिमय दर में एक प्रतिशत का अंतर कुल निजी निवेश को भी एक प्रतिशत से अधिक तक प्रभावित करता है। यानी वास्तविक विनिमय दर में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी निजी निवेश को 15 प्रतिशत तक हतोत्साहित करेगी। विनिमय दर में जितना इजाफा होगा, निर्यात उतना ही कम प्रतिस्पर्धी होता जाएगा और आयात को बढ़ावा मिलेगा। ये दोनों ही कारक निजी निवेश को प्रभावित करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट क्षेत्र पर इसका असर गैर कॉर्पोरेट क्षेत्र की तुलना में अधिक होता होगा। यह कॉर्पोरेट निवेश को 2.6 फीसदी तक प्रभावित करेगा। कॉर्पोरेट निवेश में आई कमी को इससे समझा जा सकता है।
निजी निवेश को स्पष्टï करने वाला एक और अहम कारक है जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी। निजी ऋण से जीडीपी में प्रतिशत में होने वाले बदलाव का अनुपात निजी निवेश को 1.3 प्रतिशत तक प्रभावित करता है। एक बार फिर कॉर्पोरेट निवेश ही अधिक प्रभावित होता है। यह प्रतिशत 2.3 तक रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गैर कॉर्पोरेट निवेश की बैंकिंग क्षेत्र के ऋण तक बहुत अधिक पहुंच नहीं है और इसके निवेश का काफी हिस्सा खुद से आता है। बैंकिंग व्यवस्था से ऋण में कमी की शुरुआत वर्ष 2010-11 में उच्च राजकोषीय घाटे की वजह से हुई। कॉर्पोरेट निवेश वर्ष 2007-08 में जीडीपी के 16 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013-14 में 9 प्रतिशत रह गई। इस अवधि में वास्तविक विनिमय दर 15 फीसदी तक बढ़ी क्योंकि देश में विदेशी पूंजी की आवक हो रही थी। खासतौर पर वैश्विक मंदी के बाद जब अमेरिका ने आर्थिक प्रोत्साहन नीति शुरू की थी। इस बीच मुद्रास्फीति बढ़ी और रुपये के अधिमूल्यन को इजाजत मिली। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बढ़ाए और इस अवधि में यह 250 अरब डॉलर तक रही।
वास्तविक विनिमय दर को जानबूझकर बढऩे दिया गया। हमारे अनुमान के मुताबिक विनिमय दर में 15 फीसदी की यह बढ़ोतरी कॉर्पोरेट निवेश को 35 प्रतिशत तक नीचे ले आई। ये तमाम कारक गैर कॉर्पोरेट निवेश को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करते और यह वर्ष 2012-13 तक मजबूत बना रहा। लेकिन इसके बाद उसमें गिरावट का दौर शुरू हो गया। हाल के दिनों में आई कुछ गिरावट के लिए धीमी वृद्घि दर को वजह माना जा सकता है लेकिन इसके लिए सार्वजनिक बुनियादी निवेश में साझा कमी भी वजह है। सार्वजनिक बुनियादी निवेश एक अहम चर है जो निजी-गैर कॉर्पोरेट निवेश को एकत्रित करने में मदद करता है। इसमें भी कमी आने लगी और वर्ष 2008-09 में जीडीपी के 3.3 प्रतिशत से कम होने के बाद यह लगातार कम बनी हुई है।
सन 1980 और 90 के दशक में अधिकांश वक्त भारत ने जीडीपी के 5 से 6 प्रतिशत तक का निवेश बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में किया जबकि चीन में यह आंकड़ा करीब 15 प्रतिशत था। भारत के उस निवेश में भी अधिकांश हिस्सा सरकारी था। तब से अब तक बुनियादी निवेश बढ़कर जीडीपी के 9 फीसदी के बराबर हो गया है लेकिन इसका दो तिहाई हिस्सा अब सरकारी नहीं बल्कि निजी क्षेत्र से आता है।
सार्वजनिक बुनियादी निवेश में गिरावट आई है और यह जीडीपी के 3 फीसदी से कम रह गया है। बहरहाल, निजी निवेश का काफी हिस्सा सरकारी बैंकों द्वारा वित्त पोषित होता है और वह परियोजनाओं के धीमे क्रियान्वयन के चलते फंसे हुए कर्ज में इजाफा कर रहा है। बैंकों द्वारा वित्त पोषित अधिकांश निजी बुनियादी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। निवेश सुधारने का एक और तरीका है यह सुनिश्चित करना कि वास्तविक विनिमय दर को बढऩे नहीं दिया जाए। बल्कि उसमें कुछ कमी लाने का प्रयास किया जाए। सार्वजनिक बुनियादी निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के 5 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। इसके लिए सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी को अधिक तेजी से बेचना होगा। इसके अलावा सरकारी बैंकों में फंसे हुए कर्ज की समस्या को तेजी से निपटाना होगा। अगर ऐसा होगा तभी निजी क्षेत्र को ऋण मिल सकेगा। नए दिवालिया कानून से भी मदद मिलेगी। भविष्य की बात करें तो सरकारी बैंकों को बुनियादी परियोजनाओं में लंबी अवधि का निवेश करने पर मजबूर करना उनकी समस्याएं बढ़ाने वाला साबित होगा।
देश की विनिवेश दर जीडीपी के 30 फीसदी से नीचे जा चुकी है जबकि हमें 35 प्रतिशत से ऊपर की विनिवेश दर की आवश्यकता है। इसमें सरकारी निवेश 8 प्रतिशत के आसपास हो जबकि निजी निवेश 27 प्रतिशत। सरकारी बुनियादी निवेश भी बढ़कर जीडीपी के 5 फीसदी से अधिक होना चाहिए जबकि कॉर्पोरेट निवेश जीडीपी के 15 फीसदी के बराबर। केवल तभी हमें वास्तविक तौर पर जीडीपी में 8-9 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
जेटली का दर्द और दवा
नडीए-2 सरकार दूसरा साल पूरा कर चुकी है और उसे विपक्ष से ही नहीं, न्यायपालिका से भी गुरेज है कि राजकाज में दखलअंदाजी उसके कदम रोक रही है। खासकर हाल में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कायरे से संबंधित निर्देश में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस सरकार के इकलौते कर्णधार, वित्त मंत्री अरुण जेटली को नागवार गुजरा कि सरकार आपदा राहत में नाकामी की जवाबदेही ले और एक कोष की स्थापना करे जिससे पीड़ितों को राहत मुहैया हो सके। जेटली के मुताबिक यह बजट निर्माण और विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप की तरह है। वे लगातार कह रहे हैं कि न्यायपालिका को नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य सभा के आखिरी बैठकों में उन्होंने तो यहां तक कहा कि न्यायपालिका जिस तरह ईट-दर-ईट विधायिका और कार्यपालिका के दायरे में खिसकती आ रही है और अगर यही रवैया रहा तो एक दिन वह बजट निर्माण प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप शुरू कर देगी। जेटली बोल तो वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में यह व्यवस्था करने के खिलाफ रहे थे कि किसी कर या राजस्व बंटवारे पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो तो उसके निबटारे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटना चाहिए, लेकिन उनकी इस आवाज में विपक्ष समेत हर किसी ने हाल ही में उत्तराखंड के मामले में अदालती हस्तक्षेप से लगे केंद्र की पहल को झटके का दर्द भी पढ़ा। केंद्र सरकार को अदालती आदेश के आगे दूसरे कई मामलों में भी मुंह की खानी पड़ी है। पहले तो उसे शीर्ष अदालतों में नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के मामले में ही सर्वोच्च अदालत से तगड़ा झटका लगा था। अदालत ने आयोग गठन के संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया था। तब भी जेटली ने उसे ‘‘अनिर्वाचितों की तानाशाही’ बताया था। अब सवाल है कि क्यों न्यायपालिका सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रही है और बार-बार सरकार को शर्मिदगी झेलनी पड़ रही है। अगर सरकारी फैसले संविधान के दायरे में सर्वोच्च बौद्धिक क्षमताओं के साथ लिए जाएं तो शायद अदालतों को यह मौका नहीं मिलेगा। इस प्रसिद्ध कहावत से जेटली भी परिचित होंगे कि लोकतांत्रिक पण्राली में हमेशा वही संस्था आगे रहती है, जो खास कालक्रम में सर्वोच्च बौद्धिक क्षमता से लैस होती है और सबसे तर्कसंगत विचारों को आगे रखती है। तो, जेटली को यह समझना चाहिए कि अगर विधायिका और कार्यपालिक सर्वोच्च बौद्धिक क्षमता का निर्वाह नहीं करेगी तो इससे बचा नहीं जा सकता। यह सवाल मोदी सरकार या जेटली के सामने ही मुंह बाये नहीं खड़ा है, बल्कि समय-समय पर दूसरी सरकारें भी इससे दो-चार होती रही हैं। पूर्व यूपीए सरकार तो न्यायपालिका ही नहीं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जैसी संवैधानिक संस्था की भी आंच महसूस कर रही थी। इसलिए आपके कदम लड़खड़ाएंगे तो आपके अधिकारों में दूसरों की दखलअंदाजी बढ़ती जाएगी। अब जरा मोदी सरकार के विधायी कामकाज को ही देख लेते हैं। एनजीओ पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक पिछले दो साल में तमाम अवरोधों के बावजूद संसद में कामकाज यूपीए के दौर से ज्यादा हुआ है, लेकिन विधायी कामकाज यानी नए विधेयक लाने में सरकार का प्रदर्शन उसके मुकाबले 40 फीसद से भी कम है। इसके लिए सरकार में पीएमओ के स्तर पर बेहद केंद्रीकरण को दोषी माना जाता है। उसे विपक्ष से टंटा मोल लेने और तरह-तरह के विवादों से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। देशभक्तिऔर बीफ प्रतिबंध जैसे विवाद तो ताजा है। इन सबका असर दूसरी संस्थाओं पर पड़ता है। उत्तराखंड मामले में ही सुप्रीम कोर्ट के सवालों का तीक्ष्ण बौद्धिक जवाब वह नहीं दे पाई। सरकार की दलील इसी के इर्द-गिर्द घूमती रही कि राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। इसी तरह, वित्त मंत्री का मानना है कि बजट निर्माण और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का आवंटन पूरी तरह राजनैतिक फैसला होता है। इसलिए उसमें न्यायिक दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। बेशक, विधायिका और कार्यपालिका अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों और मूलभूत अधिकारों को ध्यान में रखकर यह सब करते हैं तो अदालतों को हस्तक्षेप की कोई वजह नहीं बनती। लेकिन, इन मूलभूत सिद्धांतों को नजरअंदाज करके राजकाज चलाना चाहते हैं तो अदालतों को हस्तक्षेप का अधिकार बनता है। मसलन, संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को जीवन जीने और आजादी का अधिकार हासिल है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस अधिकार की रक्षा करे। अगर वह आपात स्थितियों में अपने इस कर्तव्य को पूरा करने में नाकाम रहती है तो न्यायपालिका को अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप करने और राहत का उचित निर्देश देने का अधिकार है। अदालतों को बजट में आवंटन का फैसला करने का अधिकार तो नहीं है लेकिन वह इस पर टिप्पणी जरूर कर सकती है कि कहां आवंटन जरूरी है। संभव है, जेटली जी को अदालत से आधार विधेयक पर विपरीत टिप्पणी भी हासिल हो क्योंकि उसे महज राज्य सभा में विपक्ष के अड़ंगे या टिप्पणियों से बचाने के लिए धन विधेयक के रूप पारित करवा लिया गया। अगर कार्यपालिका और विधायिका खुद अपने दायरे को लांघती और मर्यादा की रेखाओं को मिटाती जा रही है तो उसे न्यायपालिका का हस्तक्षेप तो सहना ही होगा। न्यायपालिका ही क्यों, यह हस्तक्षेप आम समाज और सिविल सोसायटी की ओर से भी आ सकता है। लोकपाल के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान भी संसद या विधायिका को लेकर कई सवाल उठे थे। तब भी सरकार या सांसदों का यही कहना था कि कानून बनाना हमारा काम है, किसी और से कानून का मसौदा हम नहीं ले सकते। तो, जेटली जी ये दलीलें पुरानी हैं, आप अपना राजकाज सुधारिए तो हस्तक्षेप से भी बचेंगे, वरना समय गुजर जाएगा।
कर्मचारियों की चिंता
दिवालिया कानून कारोबार की सहूलियत बढ़ाने का वादा इस आधार पर करता है कि उससे कंपनियों को बंद करना और दूसरा कारोबार खोलना आसान हो जाएगा। इसके दूसरे मकसदों में कर्मचारियों और ऋणदाताओं के हकों की रक्षा बताया जा रहा है। वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा इसके दूसरे पहलू पर जोर देते हैं। हालांकि यह आम धारणा बनती जा रही है कि कारोबार के लिए सहूलियत मुहैया कराने के खातिर श्रमिक कानूनों को ढीला बनाने और कर्मचारियों को नौकरी पर रखने तथा हटाने की शत्रे आसान बनाने की दिशा में एनडीए ही नहीं, पूर्व यूपीए सरकार भी अग्रसर थी। खासकर नव-उदारवादी और आज के दौर के वित्तीय पूंजीवादी व्यवस्था सस्ते और आसान श्रम की शतरे पर ही आधारित हैं। इसी वजह से पूंजीवाद में ही श्रमिकों को हासिल अधिकारों पर अब खास र्चचा नहीं होती। दरअसल यह तो सही हो सकता है कि अलाभकारी उद्योगों में उन कर्मचारियों को भी ढोते रहने से नुकसान बढ़ जाता है, जिनकी उपयोगिता किन्हीं वजहों से नहीं रह गई है। लेकिन कर्मचारियों के पास सामाजिक सुरक्षा के बेहद कम उपाय होने से संकट कई गुना बढ़ जाता है। आखिर कर्मचारी हितों को ध्यान में रखना देश में रोजगार सृजन को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। अगर यह नहीं होता है और सिर्फ पूंजी निर्माण पर ही जोर रहता है तो वह स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं कहलाएगी। इसलिए मौजूदा कानून में सिर्फ इतनी भर व्यवस्था से कितना लाभ होगा, कहना मुश्किल है कि बंद की गई कंपनी की संपत्ति बिक्री से कर्मचारियों को सबसे पहले उनकी देय राशि मिलेगी। बाकी की राशि कर्जदाताओं को मुहैया करा दी जाएगी। वजह यह है कि हम खासकर करोड़ों के कर्जदार विजय माल्या के मामले में देख चुके हैं कि संपत्तियों की बिक्री का मामला आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में तो कर्मचारियों को ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सरकार को इसकी दूसरी व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए क्योंकि देश में बढ़ती बेरोजगारी के दौर में संकट और गंभीर हो सकता है। अर्थव्यवस्था में अगर संतुलन का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद हालात में सुधार नहीं लाया जा सकता। वैसे, कुछ समय से कर्मचारियों के हक की बात भी होने लगी है वरना नेताओं के मुंह से भी सिर्फ कारोबारी सहूलियत पैदा करने की ही बातें हो रही थीं।
Jaitley’s Complaint: Courts should not encroach into executive domain, governance must improve too
A sharp speech in Parliament by finance minister Arun Jaitley has once again foregrounded simmering tension between different organs of the state. According to Jaitley the judiciary was overreaching into legislative and executive domains, a sentiment which other parliamentarians – not necessarily from BJP – share. This bodes ill as the Constitution provides for a separation of powers between legislature, executive and judiciary. Democracy functions smoothly when each branch stays within established boundaries. The legislature’s anxiety is not unfounded as there have been instances when judicial verdicts have pushed the boundaries. It is imperative for the judiciary to be restrained.
In India, it is the Constitution which is supreme. It empowers legislature to make laws and judiciary to interpret them in the event of disputes and litigation. The Constitution’s architects envisaged the judiciary as a counter-majoritarian institution which would uphold it in case of deviations. The judiciary has not been passive in this role. For example, in order to enhance access it has been willing to consider even a postcard mailed to it as material enough to act. But apart from ruling on constitutional issues, judicial restraint is essential if harmonious balance between different branches of government is to be preserved.
The equilibrium can be upset when the broad-based nature of a verdict encroaches on the domain of the legislature or executive. Verdicts such as the recent one in Delhi’s air pollution case have asked for an increase in specific environmental tax. Another instance was when Supreme Court recently set a short deadline for government to create a drought mitigation fund. There are two immediate dangers of overstepping. It upsets the balance of power and triggers friction between different branches of government.
It needs to be pointed out, however, that other branches of government have not been blameless in this regard. The executive’s failures and lack of accountability have often led people to approach the judiciary to get existing laws implemented. In a similar manner, legislature has often been unresponsive to changes in society. To illustrate, the first step to provide formal protection against sexual harassment at the workplace was the outcome of judiciary stepping into a vacuum left by legislature. If democracy is to function smoothly, other branches of government too must raise their game while the judiciary exhibits restraint, keeping in mind that its job is to interpret laws not make them.