
24-03-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:24-03-25
Date:24-03-25
Justices And Justice
Judicial in-house inquiries against judges don’t have a great record. Will this time be different?
TOI Editorials
Last week’s report of firefighters finding a large stash of cash at a high court judge’s home in the nation’s capital, was highly unusual. It was also disputed, both by the judge and senior personnel of the fire department itself. Then, the Supreme Court did something even more unusual. It uploaded on its website the photos and video showing what was found. This means amidst contradictory accounts, people can see for themselves that the found articles did indeed include currency notes. Big public interest in this developing story is very understandable. Ancient Greeks put it best: it is in justice that the ordering of society is centred. This order in turn hinges on judicial rectitude. Every murmur of dishonesty runs a tremor through the whole edifice.
Per procedure, CJI Sanjiv Khanna has constituted a committee to conduct an inquiry into the corruption allegations. It’s made up of the chief justices of Punjab & Haryana HC and Himachal Pradesh HC and a Karnataka HC judge. The person they have to investigate is Justice Yashwant Varma, sitting judge of Delhi HC, who is scheduled to retire not before 2031. Nothing speaks the seriousness of their assignment more than that no HC or SC judge has ever been impeached – one judge quit midway through parliamentary debate on his conduct – or convicted for corruption in India. Are in-house judicial procedures better? Constituted in 1999, this procedure aims to preserve the independence of the judiciary as well as public faith in it.
A Jan report of the International Commission of Jurists has found this in-house procedure “insular” and even “ineffective”. The claim is underlined by noting that in 2022, the Union law minister told Parliament there were more than 1,600 complaints against HC and SC judges but no official information as to action taken on these complaints. This is of course on top of the opacity in selection of judges. Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankhar is just one of many who are once again arguing that the National Judicial Appointments Commission (NJAC) struck down as unconstitutional by SC in 2015, provided for judicial accountability more rigorously.
In its unprecedented sharing of documents related to the current case, SC has indicated a broader approach to public disclosures. As the in-house committee probes the case, it should remember that the aphorism justice must not only be done but must also be seen to be done is popular because it is profound.
Date:24-03-25
Holidays Are Meant To Refresh, Not Exhaust
ET Editorials
India’s travel and tourism industry is at a crossroads. While foreign tourists aren’t pouring in, domestic travel has seen an uptick. Reports show even the typically quiet Q4 turned into a whirlwind, with crowds flocking to the Maha Kumbh and an epic wedding season. These two events packed the three months with enough action to keep tour planners on their toes.
A February 2025 PIB report noted that the tourism sector’s contribution to GDP regained its pre-pandemic level of 5% in FY23. International tourist arrivals (ITAs) rebounded to prepandemic levels and forex earnings through tourism hit $28 bn in FY23. In the budget, GoI announced an initiative to develop 50 top tourist destinations in partnership with states, focusing on infra, easing travel woes and strengthening connectivity to key sites.
As Indians grow more affluent, many now prefer travelling abroad over exploring local destinations. Simultaneously, larger sections of the population are embracing domestic travel, flocking to religious hotspots, or opting for lavish destination weddings—both trends feeding into the narrative of booming local tourism. Yet the sector is far from content, pushing GoI to ramp up efforts to promote India as a global travel destination. The answer, however, to India’s flagging low international allure lies beyond marketing. Persistent issues like poor air quality, tourists being overcharged, mounting congestion, lack of cleanliness, inefficient systems, security concerns and rising costs paint a less-than-inviting picture. If India feels like hard work, travellers will go elsewhere. Only segments without alternatives—like religious tourism and grand Indian weddings—will continue to grow while other opportunities quietly slip away.
Not the only path
A purely militaristic solution against the Maoists can also lead to tribal repression
Editorial
In two operations in Bastar, Chhattisgarh on Thursday, 30 alleged “Maoists” were gunned down taking the number of Maoists killed in operations, according to security forces, to over 100 this year. In its 20-plus years of existence as a unified political force, the Communist Party of India (Maoist) finds itself in its most challenging period. The insurgency had peaked in the mid- to late-2000s, when the then government termed it as the “greatest security threat” to the nation, and has since then been restricted to the forested areas of southern Chhattisgarh and contiguous areas. This weakening was never in doubt — the Maoists profess an anachronistic political strategy of adopting violent means to achieve their goals, and in the long war of attrition against the Indian state, have subjugated their “mass” work to militarism. This has resulted in the erosion of support bases in places that were built where and when the agencies of the Indian state were weak. With successive central governments seeking to address the development lacunae in governance in such tribal areas and adopting a take-no-prisoners approach to tackle the Maoists’ guerilla warfare, their threat has been significantly whittled down. In the anti-insurgency strategy, however, the police and paramilitary agencies have made errors — the Salwa Judum campaign is one example and it is still not clear whether the anti-Maoist operations that have led to claims of many casualties among the insurgents include tribals caught in the crossfire.
If the Indian state — the Union and State governments — believes that the Maoist threat can be extinguished using a purely militaristic approach, then this is not borne out from experiences elsewhere against similar insurgencies. Ideologies such as Maoism, even if anachronistic and misplaced in the current socio-political milieu, tend to take deeper roots when repressions peak and a purely militaristic solution that envisages a violent end to the insurgency has the possibility of causing disenchantment among tribals. A better solution would be to involve civil society in working out a truce and sending a clear message for the Maoists to give up their violent path with incentives for rehabilitation. The Maoists have shown little inclination in doing so, being stubborn in upholding their flawed understanding of the Indian state and the people. The loss of lives, that includes tribals either coerced into the violence due to repression that they face or simply caught in the crossfire, should compel them to change tack, if they are truly concerned about the lot of the tribal people they claim to stand up for. The experience of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) or that of the Nepali Maoists, who gave up their insurgent campaigns, suggests that such a pathway is possible.
बांग्लादेश से रिश्ते
संपादकीय
बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद वहां की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस की ओर से बैंकॉक में आयोजित होने वाले बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात का आग्रह यह आभास कराता है कि वह संबंध सुधार के इच्छुक हैं, लेकिन इसके प्रति सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता।
इसलिए नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि बांग्लादेश में भारत विरोधी वातावरण तैयार किया जा रहा है। वहां हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाओं पर भारत की तमाम चिंताओं के बावजूद गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। एक अन्य चिंताजनक तथ्य यह है कि कट्टरपंथी एवं जिहादी ताकतों को सहयोग, समर्थन और संरक्षण दिया जा रहा है।
अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में यूनुस ने कई कट्टरपंथी संगठनों से प्रतिबंध हटाया है और आतंकी गतिविधियों के लिए आरोपित नेताओं को जेल से रिहा भी किया है। भारत इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ता दिख रहा है।
स्पष्ट है कि यदि भारतीय प्रधानमंत्री बैंकाक में यूनुस से वार्तालाप करते हैं तो उन्हें उनके इरादों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। यूनुस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अवश्य हैं, लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर उनका कार्य व्यवहार चिंतित करने वाला है। वह यथाशीघ्र चुनाव कराने में रुचि दिखाने के बजाय ऐसे एजेंडे अपने हाथ में ले रहे हैं, जिससे लंबे समय तक सत्ता में बना रहा जाए।
अब तो बांग्लादेश की सेना भी उनके रवैये को लेकर सशंकित दिख रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरुद्ध जिन छात्रों के विद्रोह के चलते यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने, उन छात्रों ने पिछले दिनों नेशनल सिटिजंस पार्टी नाम से अपना अलग दल गठित कर लिया और यह आरोप भी लगाया कि सेना शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को फिर से सत्ता में लाने की साजिश रच रही है।
यह चकित करने वाला घटनाक्रम है। इसलिए और भी, क्योंकि बांग्लादेश की सेना ने इस पार्टी के आरोपों को हास्यास्पद और निराधार करार दिया। भारत को बांग्लादेश के घटनाक्रम पर इसलिए निगाह रखनी होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि छात्रों की इस नई पार्टी के गठन के पीछे यूनुस का ही हाथ है।
फिलहाल यह कहना कठिन है कि बैंकॉक में यूनुस और पीएम मोदी की भेंट होती है या नहीं, लेकिन भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक तो बांग्लादेश के हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा हो और दूसरे, वहां सक्रिय भारत विरोधी तत्वों पर लगाम लगे।
इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ कई बार आवाज उठाई है, क्योंकि तथ्य यह है कि वहां की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों के दमन को रोकने के लिए वांछित कदम उठाने से इनकार कर रही है।
Date:24-03-25
वैश्विक व्यापार में नए समीकरण
आदित्य सिन्हा, ( लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं )
यह 2013 की बात है। एक जापानी कंपनी ने भारत में अपने एसी बेचना शुरू किया। उसके एसी की कीमत स्थानीय प्रतिस्पर्धियों से कम थी। इसमें एक पेच था। इन एसी का निर्माण तो चीन में हुआ था, लेकिन भारत में ये मलेशिया के जरिये आते थे। विनिर्माता कंपनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए उस देश को माध्यम बनाया जिसके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए था।
चूंकि चीनी उत्पादों के लिए टैरिफ लागू था तो चीन से उत्पादों को सीधे भारत भेजने पर लागत बढ़ सकती थी। इसके लिए बस पैकेजिंग या असेंबलिंग में कुछ हेरफेर करना था और भारत में लगभग शुल्क मुक्त उत्पाद भेजना संभव था। यह एक चतुराई भरा दांव था। पूरी तरह से वैध होते हुए भी यह व्यापार नीति में विसंगतियों को रेखांकित करने वाला रहा और यह कोई इकलौता मामला भी नहीं था।
पूरे एशिया में निर्यातक एफटीए के पिछले दरवाजे से भारतीय बाजार में पैठ बनाने की जुगत में जुटे थे। इसमें अक्सर देसी विनिर्माताओं के हितों पर आघात होता रहा। समस्या उक्त विसंगति से भी गहरी है। भारत के तमाम व्यापार समझौते विशेषकर 2014 से पहले ऐसे जो अनुबंध हुए, वे रणनीतिक एवं आर्थिक तर्कों के आधार पर नहीं हुए थे।
इस दौरान साफ्टा, जीएसटीपी और श्रीलंका एवं चिली जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए गए जहां फार्मा, पूंजीगत वस्तुएं और भारी मशीनरी जैसे प्रमुख भारतीय निर्यातों के लिए तो कोई खास मांग नहीं थी, लेकिन वे भारत में चीनी सामान खपाने के परोक्ष ठिकाने जरूर बन गए।
इससे देश में आयात बढ़ते गए और भारत ने लाभ के उद्देश्य से जो समझौते किए वे दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले एकतरफा अनुबंध बनकर रह गए। इस समस्या की जड़ ‘रूल्स आफ ओरिजिन’ यानी वस्तु के मूल स्थान से संबंधित लचर नियमन में थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने इस समस्या को चिह्नित किया और व्यापार समझौतों के प्रति भारत का दृष्टिकोण बदला।
अब उन समझौतों पर जोर दिया जा रहा है जिसमें दोनों पक्षों को बराबर लाभ हो। इसके लिए सरकार किसी जल्दबाजी में भी नहीं दिखती और पूरा समय लेकर आगे बढ़ रही है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और आस्ट्रेलिया के साथ एफटीए में यही व्यापक दृष्टिकोण झलकता है।
भारत अब यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और यहां तक कि अमेरिका के साथ भी ऐसे ही किसी समझौते पर सक्रियतापूर्वक बातचीत कर रहा है। यह व्यापार नीति के पुनर्संयोजन को रेखांकित करता है, जिसमें रक्षात्मक रुख के बजाय रणनीतिक लाभ को माध्यम बनाकर आर्थिक कायाकल्प की जमीन तैयार की जा रही है।
यूएई और आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते इस दिशा में भारत के नए सोच के परिचायक हैं। इन पर साल भर से कम की वार्ता में मुहर लग गई और इनमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनमें भारत निर्यात के लिहाज से मजबूत है। यूएई ने भारत के करीब 90 प्रतिशत निर्यातों पर टैरिफ खत्म कर दिया है जिसमें रत्न एवं आभूषण, कपड़ा और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे उत्पाद शामिल हैं।
ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते से भारतीय दवा, कपड़ा और आईटी सेवाओं की एक बड़े बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए डेरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र को संरक्षण भी प्रदान किया गया। ये समझौते केवल टैरिफ में कटौती तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इन्हें इस प्रकार आकार दिया गया कि संभावनाशील बाजारों में पैठ बनाने के साथ ही घरेलू हितधारकों के हितों की भी रक्षा की जा सके।
वहीं, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और अगर अमेरिका को भी जोड़ लें तो इन पक्षों के साथ व्यापार समझौतों में इन बाजारों की प्रकृति एवं स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये सभी धनी और स्थापित मानदंडों से जुड़े बाजार हैं जहां भारतीय उत्पादों को ऊंचे दाम मिलना संभव है। इन बाजारों में पैठ से भारतीय उत्पादकों को अपनी समूची वैल्यू चेन को समृद्ध करने का अवसर मिलेगा। उन्हें गुणवत्तापरक मानकों पर खरा उतरने के लिए अपेक्षित प्रयास करने होंगे।
यह व्यापार कूटनीति में रणनीतिक दृष्टिकोण के प्रवर्तन को दर्शाता है जो वस्तुओं के परे भी तमाम पहलुओं को समाहित करने वाला है। इनमें सेवाएं, डिजिटल व्यापार, निवेश प्रवाह और नियामकीय सहयोग जैसे बिंदुओं को भी जोड़ा जा रहा है। भारत के सेवा क्षेत्र एवं उभरते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए ये महत्वपूर्ण हैं।
ये न केवल निर्यात, अपितु नवाचार, हरित प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखला सामर्थ्य की दृष्टि से भी अहम हैं। चूंकि कोविड-19 के बाद चीन संबंधी जोखिम बढ़ने के साथ ही वैश्विक व्यापार की दशा-दिशा काफी बदली है तो भविष्य को देखते हुए यह भारत के लिए व्यापक अवसरों के द्वार खोलने की क्षमता रखते हैं।
इस चर्चा में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब विश्व में बहुपक्षीय व्यापार और संस्थान दबाव में हैं तब आखिर क्यों दुनिया के तमाम देश भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को और गहरा करने में दिलचस्पी रखते हैं। यह रणनीतिक एवं आर्थिक, दोनों प्रकार के आकलनों को दर्शाता है।
असल में भारत का बढ़ता उपभोक्ता आधार, तेजी से बढ़ता मध्य वर्ग और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की संभावनाओं ने भारत को एक आकर्षक व्यापार साझेदार के रूप में स्थापित किया है। साथ ही साथ वैश्विक कंपनियां आपूर्ति शृंखला निर्भरता के भी नए सिरे से आकलन में जुटी हैं। इस परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी श्रम लागतों, औद्योगिक नीति सुधारों और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के दम पर भारत एक भरोसेमंद वैकल्पिक विनिर्माता के रूप में उभर रहा है।
वैश्विक व्यापारिक मोर्चे पर ये नए समीकरण भारत को केवल आर्थिक लाभ ही नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसे साझेदारों के साथ बढ़ती कदमताल से आपूर्ति शृंखला के विविधीकरण और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक सक्रियता को गति मिलने से देश के सामरिक हितों की भी पूर्ति होगी। ऐसे में भारत को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हरसंभव प्रयास करने चाहिए। इस दिशा में आर्थिक सुधारों सहित भारत सरकार की कोशिशें अब कुछ रंग लाती दिख रही हैं।
जांच की जरूरत
संपादकीय
दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी निवास से भारी मात्रा में नगदी प्राप्त होने के बाद देश के प्रधान न्यायाधीश ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनको न्यायिक कामकाज से अलग रखने को कहा। साथ ही इन अरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया। जैसा कि जस्टिस वर्मा के घर होली वाले दिन लगी आग पर काबू पाने गए अग्निशमन कर्मचारियों को स्टोर रूम में भारी नकदी मिली थी। इलाहाबाद बार एशोसिएशन ने इसे पंद्रह करोड़ रुपये बताया। पुलिस के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से आग की घटना के दौरान की सभी कॉल्स को सुरक्षित रखने को कहा है। पिछले छह महीनों के उनके कॉल रिकार्ड भी अदालत ने पुलिस से मांगे हैं। शीर्ष अदालत ने पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो, तस्वीरें व शुरुआती जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। जस्टिस यशवंत का दावा है कि उन्होंने खुद या उनके परिवार ने कभी नकदी नहीं रखी, यह उनके खिलाफ साजिश है। खबरों के अनुसार उनके आवास में मौजूद सुरक्षाकर्मी ने माना कि अग्निकांड की अगली सुबह कुछ अधजली चीजों को वहां से हटाया गया। जो है मामले को और भी संदिग्ध बना रहा है। जांच रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि घर के इस हिस्से में घरवालों के अलावा नौकरों व मालियों का भी आना-जाना था । कहा जा सकता है कि यूं असुरक्षित व खुले में इतनी मोटी राशि रखने का औचित्य नहीं बनता। मगर पिछले दिनों इनकम टैक्स के छापों में पुरानी-खटारा खड़ी गाड़ी में भारी नकदी पाए जाने जैसी घटनाओं का याद आना स्वाभाविक है। उनके निवास में लगे सभी सीसीटीवी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। न्याय की कुर्सी पर बैठे शख्स से बेदाग होने की उम्मीद बेमानी नहीं कही जा सकती। सबसे बड़ी अदालत ने 1999 में इन-हाउस कमेटी का गठन किया था, जिसमें तीन जजों की कमेटी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ हुई शिकायतों की जांच करती है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस जली हुई राशि व जज का सिर्फ तबादला किये जाने पर काफी रोष व्यक्त किया था, जो न्याय- व्यवस्था पर सीधा प्रहार था। निःसंदेह निष्पक्ष जांच द्वारा ही दूध का दूध पानी का पानी किया जा सकता है। जज के बेकसूर पाए जाने के बाद भी जरूरी है, साजिश की गहराई से पड़ताल की जाए दोषी पाए जाने पर कमेटी इस्तीफे की मांग भी कर सकती है। न्यायपालिका की निष्पक्षता को अक्षुण्य बनाये रखने के हर संभव प्रयास जरूरी हैं।
Date:24-03-25
वरदान था या चुनौती ?
विनीत नारायण
सुनीता विलियम्स की वापसी से सारी दुनिया ने राहत के सांस ली है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर नौ महीने से अधिक समय बिताकर सुर्खियां बटोरीं। यह यात्रा, , जो मूल रूप से केवल आठ दिनों के लिए नियोजित थी, बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी के कारण अनपेक्षित रूप से लंबी हो गई। 5 जून 2024 को शुरू हुई यह यात्रा 19 मार्च 2025 को समाप्त हुई, जब वे पृथ्वी पर लौटीं इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं: क्या सुनीता का यह लंबा अंतरिक्ष प्रवास एक वरदान था या यह एक चुनौतीपूर्ण अनुभव था जिसने उनके जीवन और विज्ञान को नये आयाम दिए? आज इस प्रश्न का हम गहराई से विश्लेषण करेंगे।
सुनीता और उनके सहयोगी बुच विल्मोर को बोइंग स्टारलाइनर के पहले मानवयुक्त परीक्षण मिशन के तहत आईएसएस पर भेजा गया था। योजना थी कि वे आठ दिन वहां रहकर अंतरिक्ष यान की कार्यक्षमता का परीक्षण करेंगे और वापस लौट आएंगे, लेकिन स्टारलाइनर के अस्टर्स में खराबी और हीलियम रिसाव जैसी समस्याओं ने उनकी वापसी को असंभव बना दिया। नासा ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्टारलाइनर को बिना चालक दल के पृथ्वी पर वापस भेजा और सुनीता विलियम्स को आईएसएस पर ही रहने का निर्णय लिया। इस तरह उनका आठ दिन का मिशन नौ महीने की लंबी यात्रा में बदल गया।
सुनीता का यह लंबा प्रवास विज्ञान के लिए एक अनमोल अवसर साबित हुआ। आईएसएस पर रहते हुए उन्होंने 150 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें 900 घंटे से ज्यादा समय रिसर्च में बिताया। इन प्रयोगों में जल पुनर्चक्रण प्रणाली, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में बैक्टीरिया और यीस्ट की जैव-उत्पादन प्रक्रिया और अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में सामग्रियों के पुराने होने जैसे अध्ययन शामिल थे। ये शोध भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों, विशेष रूप से मंगल ग्रह जैसे लंबी अवधि के अभियानों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, पैक्ड बेड रिएक्टर एक्सपेरिमेंट (PBRE-WRS) में
सुनीता ने जल पुनर्जनन प्रणाली की जांच की, जो यह समझने में मदद करती है कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में जल शोधन कैसे काम करता है। यह तकनीक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पानी की आपूर्ति को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो सकती है। इसी तरह, यूरो मटेरियल एजिंग प्रयोग ने अंतरिक्ष यान और उफाहों के डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए डेटा प्रदान किया। इस दृष्टिकोण से देखें तो उनका लंबा प्रवास न केवल नासा के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक वरदान था, क्योंकि इससे प्राप्त ज्ञान अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देगा। सुनीता विलियम्स पहले से ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं। उन्होंने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा (2006-07) में 29 घंटे से अधिक का स्पेसवॉक करके महिलाओं के लिए रिकॉर्ड बनाया था। इस बार नौ महीने के प्रवास के दौरान उन्होंने कुल 62 घंटे और 9 मिनट का स्पेसवॉक पूरा किया, जिससे वह अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेसवॉक करने वाली महिला बन गईं। यह उपलब्धि उनके धैर्य, साहस और समर्पण का प्रतीक है।
इसके अलावा, वे अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला भी बन गई। यह रिकॉर्ड न केवल उनके कॅरियर का एक सुनहरा पन्ना है, बल्कि यह दुनिया भर की महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि कठिन परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की जा सकती है। मानसिक रूप से भी यह यात्रा आसान नहीं थी। परिवार से दूर, एक सीमित स्थान में नौ महीने बिताना भावनात्मक तनाव पैदा कर सकता है। हालांकि, सुनीता ने
इंटरनेट कॉल के जरिए अपने पति मां और परिवार से संपर्क बनाए रखा, जिससे उन्हें भावनात्मक सहारा मिला। फिर भी, अनिश्चितता और अलगाव की भावना उनके लिए एक बड़ी चुनौती रही होगी। इस दृष्टिकोण से, यह अनुभव एक वरदान कम और एक कठिन परीक्षा अधिक लगता है। सुनीता का यह अनपेक्षित ठहराव अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण सबक भी लेकर आया। बोइंग स्टारलाइनर की तकनीकी खामियों ने यह सवाल उठाया कि क्या निजी कंपनियां अंतरिक्ष यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
इस घटना ने नासा को स्पेसएक्स जैसे वैकल्पिक विकल्पों पर निर्भरता बढ़ाने के लिए मजबूर किया, जिसके ड्रैगन यान ने अंततः सुनीता और बुच को वापस लाया। यह अनुभव अंतरिक्ष यानों की विश्वसनीयता, सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन योजनाओं को बेहतर करने की जरूरत को रेखांकित करता है। इस तरह, यह घटना भविष्य के मिशनों को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। भारत के लिए सुनीता विलियम्स का यह सफर विशेष रूप से गर्व का विषय है। गुजरात के अहमदाबाद से संबंध रखने वाली सुनीता ने न केवल अपनी उपलब्धियों से, बल्कि अपनी दृढ़ता से भी भारतीय युवाओं को प्रेरित किया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि तकनीकी बाधाएं और व्यक्तिगत चुनौतियां भी इंसान को अपने लक्ष्य से नहीं रोक सकतीं। भारत जैसे देश में, जहां अंतरिक्ष अनुसंधान तेजी से बढ़ रहा है (जैसे गगनयान मिशन), सुनीता का यह अनुभव एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकता है।
इस नजरिए से उनका नौ महीने का प्रवास भारत के लिए भी एक अप्रत्यक्ष वरदान है। सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में नौ महीने का प्रवास एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक और यह वैज्ञानिक प्रगति, व्यक्तिगत उपलब्धियों और भविष्य के मिशनों के लिए सबक लेकर आया, जो इसे एक वरदान बनाता है। दूसरी ओर, शारीरिक और मानसिक चुनौतियों ने इसे एक कठिन अनुभव बनाया, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। शायद सच्चाई यह है कि यह दोनों का मिश्रण था- एक ऐसा वरदान जो कठिनाइयों के साथ आया और एक ऐसी चुनौती जो अनमोल अवसरों में बदल गई। सुनीता की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में अप्रत्याशित परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हों, उनसे कुछ न कुछ सकारात्मक हासिल किया जा सकता है।
तापमान की चुनौती
संपादकीय
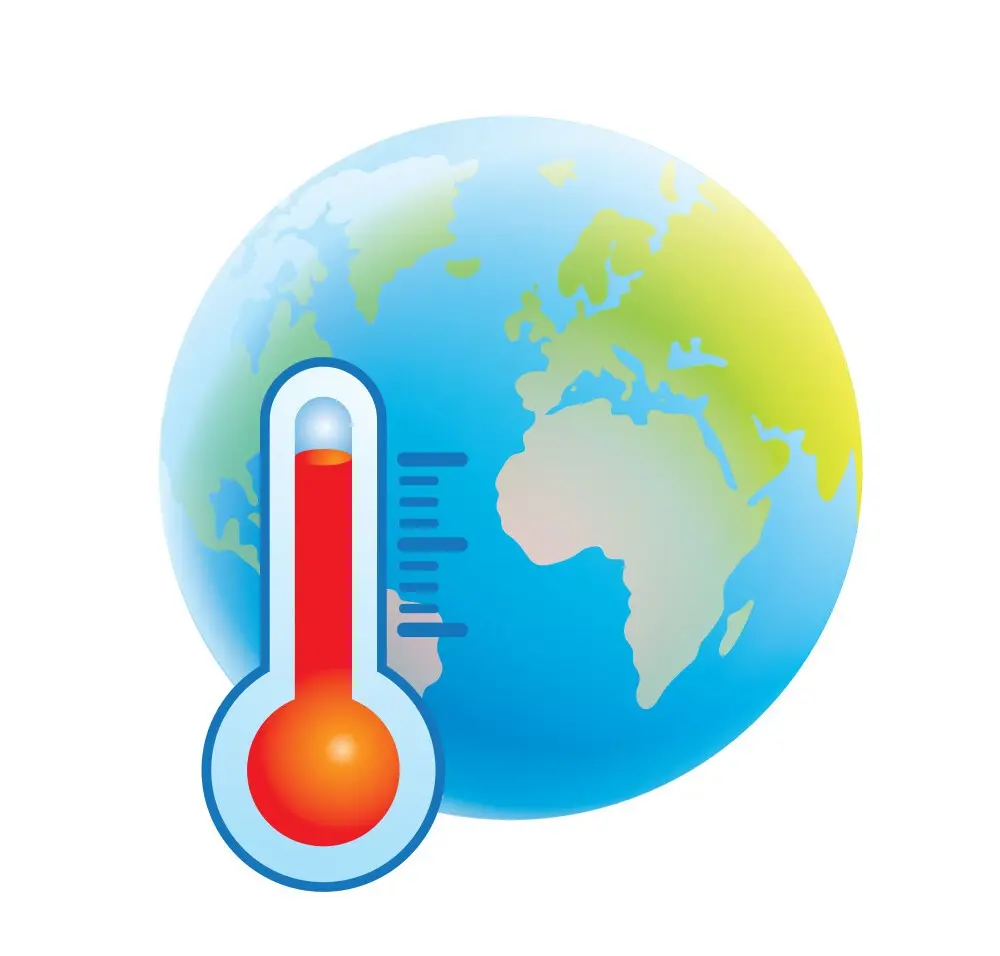
भारत में मौसम की चिंता बढ़ती चली जा रही है। कुछ इलाकों में बारिश का आलम है, तो अनेक इलाकों में गर्मी का प्रकोप भी बढ़ गया है। मार्च के महीने में ही भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग को मार्च में ही हीटवेव अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। मध्य मार्च में ही ओडिशा में पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। विशेषज्ञ इस उछाल का कारण जलवायु परिवर्तन, मौसम के बदलते पैटर्न, स्थलीय वार्मिंग और शहरीकरण को मानते हैं। बीती फरवरी 124 वर्षों में सबसे गर्म रही है और मार्च भी पहले से और गर्म साबित होने वाला है। पता नहीं, इस साल गर्मी जब अपने चरम पर पहुंचेगी, तब पारा कहां होगा? एक नए अध्ययन में पाया गया है कि भारत के कुछ शहर हीटवेव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, पर वे मुख्य रूप से अल्पकालिक प्रतिक्रियाओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि गर्मी से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपाय जरूरी होते जा रहे हैं। यह अध्ययन नई दिल्ली स्थित एक शोध संगठन ‘सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव’ ने जारी किया है।
शोध में इस बात की जांच की गई है कि नौ प्रमुख भारतीय शहर- बेंगलुरु, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर, कोटा, लुधियाना, मेरठ, मुंबई और सूरत, बढ़ती गर्मी के लिए कैसी तैयारियां कर रहे हैं? इन शहरों में भारत की शहरी आबादी का 11 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रहता है।
इस अध्ययन ने भविष्य की गर्मी की चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की जरूरत पर बल दिया है। हकीकत यह है कि इन शहरों के जिम्मेदार अधिकारी बढ़ती गर्मी को लेकर गंभीर नहीं हैं। वे फौरी फैसलों के दम पर ही मौसम की अति से जूझते आ रहे हैं। हमारे शहरों ने मौसम की अति से बचने के लिए जरूरी उपाय नहीं किए हैं और दीर्घकालिक कदमों का अभाव है। अगर शहरों ने अपने आपको अत्यधिक गर्मी से जूझने के लिए तैयार नहीं किया, तो फिर प्रभावी दीर्घकालिक रणनीति के अभाव में देश को आने वाले वर्षों में लगातार तीव्र और लंबे समय तक चलने वाली गर्मी की लहरों के चलते जान-माल के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वास्तव में, हम तापमान से लड़ने के उपाय करने में पिछड़ गए हैं, जबकि हमारे शहरों की आबादी दिनों-दिन बढ़ती चली जा रही है। यदि हमने दीर्घकालिक उपायों की शुरुआत अब भी की, तो लाभ पाने में कई वर्ष लग जाएंगे। फिर भी युद्ध स्तर पर प्रयासों की जरूरत है। किंग्स कॉलेज, लंदन के एक वरिष्ठ शोधकर्ता आदित्य बलियाथन पिल्लई बताते हैं कि आने वाले दशकों में मृत्यु दर और आर्थिक क्षति में ज्यादा वृद्धि को रोकने के लिए बचाव के उपायों को तत्परता से लागू किया जाना चाहिए।
अध्ययन में यह बताया गया है कि हमारे ज्यादातर शहर पेयजल के इंतजाम में भी पीछे चल रहे हैं। गांव की बात दूर है, शहरों में श्रमिकों के लिए काम के स्थान पर शीतलता सुनिश्चित करने के उपाय में भी हम पीछे हैं। बेहतर अग्नि प्रबंधन और पावर ग्रिड विकास जैसे उपायों का भी अभाव है। पेड़ लगाने और छत पर सौर ऊर्जा लगाने में भी हम पर्याप्त रूप से आगे नहीं हैं। शहरों को गर्मी के दुष्प्रभाव को रोकना होगा, अभी केवल लू के शिकार लोगों की सेवा पर जोर दिया जाता है। इस उपयोगी अध्ययन ने इशारा किया है कि तापमान जनित आपदा से निपटने के लिए सरकारी विभागों के बीच समन्वय का अभाव है, पर सबसे बड़ी जरूरत है, लोगों का जागरूक होना।
Date:24-03-25
तपेदिक से लड़ाई में निर्णायक मोड़ पर
जगत प्रकाश नड्डा, ( केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री )
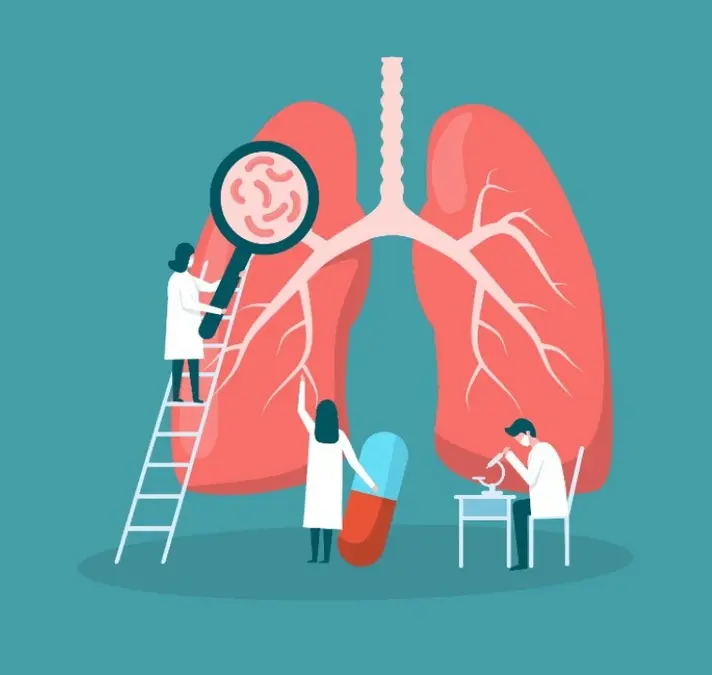
आज विश्व तपेदिक (टीबी) दिवस है। इस अवसर पर मैं बहुत गर्व के साथ बता सकता हूं कि इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में भारत किस तरह से अपनी सफल रणनीति का नया अध्याय लिख रहा है। हाल ही में संपन्न * 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान’ ने न केवल नवाचार की शक्ति का प्रदर्शन किया है, बल्कि यह भी दिखाया कि समुदायों को संगठित करने का कार्यक्रम इस बीमारी से प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलने में कितना महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। यह अभियान 7 दिसंबर, 2024 को टीबी के मामलों का पता लगाने में तेजी लाने, मृत्यु दर को कम करने और नए मामलों को रोकने के उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था।
इस अभियान ने टीबी का जल्द पता लगाने के लिए अत्याधुनिक रणनीति अपनाई, जिनसे यह सुनिश्चित हुआ कि बिना लक्षण वाले मरीजों की भी पहचान हो सके और फिर उनका फौरन इलाज शुरू किया गया। अन्यथा उनका उपचार ही नहीं हो पाता। पोर्टेबल एक्स- रे मशीनों को उच्च जोखिम वाले लोगों के पास ले जाया गया, जिनमें मधुमेह, धूम्रपान करने वाले, शराब पीने वाले, एचआईवी संक्रमित बुजुर्ग और टीबी के रोगियों के घरेलू संपर्क में रहने वाले लोग शामिल थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से संचालित एक्स-रे ने संदिग्ध टीबी मामलों को तुरंत चिह्नित किया, फिर न्यूक्लिक एसिड एम्प्लिफिकेशन टेस्ट (नात) का उपयोग करके मामलों की पुष्टि की गई और उनका जल्दी से इलाज किया गया, जिससे संक्रमण पर लगाम लगी और लोगों की जान बचाई गई।
यह अभियान देश के कोने-कोने तक पहुंचा, जिसके तहत टीबी हो सकने के जोखिम वाले 2.97 करोड़ लोगों की जांच की गई। इस गहन प्रयास के कारण 7.19 लाख टीबी रोगियों की पहचान की गई। इनमें से 2.85 लाख मामले बिना लक्षण वाले थे और इस अभिनव दृष्टिकोण के बिना वे छूट जाते। इस कदम से टीबी संक्रमण की श्रृंखला टूट गई। यह सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि इस रोग के उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी है।
भारत से टीबी उन्मूलन अब जन भागीदारी द्वारा संचालित एक जन आंदोलन है। पूरे भारत में 13.46 लाख से ज्यादा निक्षय शिविर आयोजित किए गए, जिनका सांसदों, विधायकों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों सहित 30,000 से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने समर्थन किया। कॉरपोरेट जगत व नागरिकों की भागीदारी से यह विचार मजबूत हुआ है कि टीबी उन्मूलन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सामूहिक मिशन है।
इस मिशन में जन भागीदारी के अनूठे उदाहरण देखने को मिले। 22 संबंधित मंत्रालयों में टीबी जागरूकता, पोषण किट वितरण, टीबी मुक्त भारत के लिए शपथ लेने जैसी 35,000 से ज्यादा गतिविधियां आयोजित की गई। इसी तरह, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, व्यापार संघों, व्यावसायिक संघों, स्वैच्छिक संगठनों के साथ 21,000 से अधिक गतिविधियां की गई और 78,000 शैक्षणिक संस्थानों में 7.7 लाख से अधिक छात्र- छात्राओं ने टीबी जागरूकता और संवेदीकरण गतिविधियों में भाग लिया। विभिन्न जेलों, खदानों, चाय बागानों, निर्माण स्थलों और कार्य स्थलों पर 4. 17 लाख से अधिक संवेदनशील आबादी की स्क्रीनिंग की गई। अभियान अवधि के दौरान त्योहारों पर 21,000 से अधिक टीबी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें धर्मगुरुओं और विभिन्न समुदायों के प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण ने इस भागीदारी की आधारशिला रखी है। न केवल पोषण, बल्कि मनो- सामाजिक व व्यावसायिक समर्थन के लिए रोगियों को गोद लेने के वास्ते व्यापक सामाजिक समर्थन जुटाया गया। टीबी रोगियों के लिए सहायता अब अस्पतालों तक सीमित नहीं है, यह घरों, गांवों और कार्यस्थलों पर भी हो रही है। निक्षय मित्र पहल के माध्यम से व्यक्ति और संगठन टीबी पीड़ित परिवारों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस पहल में हजारों पोषण किट पहले ही वितरित की जा चुकी हैं। सिर्फ 100 दिनों में 1,05,181 नए निक्षय मित्रों को पंजीकृत किया गया। पोषण और टीबी से उबरने के बीच महत्वपूर्ण संबंध को देखते हुए सरकार ने निक्षय पोषण योजना के
तहत वित्तीय सहायता को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी टीबी रोगी इस लड़ाई को अकेले न लड़े। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी टीबी रोगियों के लिए विभेदित टीबी देखभाल कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत उपचार प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिए, यह निर्देशित किया गया है कि यदि किसी टीबी रोगी का वजन कम पाया जाता है, तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता उसके लिए अनुकूलित पोषण और उपचार योजना तैयार करेंगे और हर महीने उसकी प्रगति की निगरानी करेंगे।
इस अभियान की गति ने यह भी दर्शाया है कि समाज और सरकार का समग्र दृष्टिकोण कैसा परिवर्तनकारी बदलाव ला सकता है। टीबी के प्रति जागरूकता और सेवाओं को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने के लिए 22 मंत्रालयों ने मिलकर काम किया। देश भर के स्कूलों में टीबी जागरूकता संदेशों को सुबहकी सभाओं में शामिल किया गया। लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने तो हजारों आगंतुकों को मुफ्त टीबी जांच की पेशकश करने के लिए अपने क्लस्टर कार्यालयों के नेटवर्क का लाभ उठाया। इन विविध प्रयासों ने टीबी से जुड़ी वर्जनाओं को तोड़ दिया और सही सूचनाओं के साथ टीबी उन्मूलन को सार्वजनिक चेतना के केंद्र में ला दिया।
यह 100 दिवसीय अभियान तो अभी शुरुआत है। भारत इन प्रयासों को पूरे देश में बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरेक नागरिक की चाहे वह कहीं पर भी रहता हो, आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण इलाज और अटूट सामुदायिक समर्थन तक पहुंच बन सके। जिस तरह भारत ने कोविड- 19 की जांच को तेजी से आगे बढ़ाया, उसी तरह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय टीबी उन्मूलन के अगले चरण में निवेश कर रहा है, ताकि अंतिम छोर तक तेज और सटीक जांच हो सके ।
चाहे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता हो या हमारे पोलियो उन्मूलन अभियान की, भारत ने पहले भी समुदाय संचालित कार्रवाई की शक्ति देखी है, अब टीबी मुक्त भारत अभियान आम लोगों के नेतृत्व वाला एक और आंदोलन बन रहा है। दरअसल, जब नवाचारों की पहुंच बनती है और सरकारें, समुदाय व व्यक्ति एकजुट होते हैं, तब असंभव भी वास्तविकता बन जाता है। भारत टीबी से सिर्फ लड़ नहीं रहा है, हम इसे हरा भी रहे हैं।