
24-03-2021 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:24-03-21
Date:24-03-21
Wrong Diagnosis
A regulatory framework that clubs social media with news platforms doesn’t work
TOI Editorials
A free press is one of the pillars of democracy. The NDA government has upheld this view. Yet, an executive order passed last month undermines this principle. The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules aim to regulate content in digital platforms. Invoked without consulting stakeholders, the order force fits news media with social media platforms. This doesn’t make sense as these two platforms are fundamentally different. Consequently, they operate on entirely different lines, making a common regulatory framework meaningless.
The most worrisome dimension of the specifics of the executive order is that it gives the bureaucracy extraordinary powers to meddle with content on flimsy grounds. It sets the stage for an inspector raj in the functioning of media which is the antithesis of a free press. In addition, the mechanism of complaint redressal prescribed by the executive order will escalate compliance costs for media platforms. The redressal mechanism, which is based on a three-tier system, requires media companies to have a time-bound response system. This approach not only introduces new compliance costs but also opens the door to harassment through a deluge of frivolous complaints, all of which need to be addressed in a short span of time.
India’s media operates in a regulated environment, which includes statutory legislation. The Press Council of India, which is headed by a retired Supreme Court judge, is responsible for setting professional standards. The government has indicated that the digitisation of news delivery requires a relook at the regulatory framework. If that’s the case, it should heed the suggestion of the Editors’ Guild. It should leave the news media out of a regulatory framework that aims to curb fake news on social media. Instead, it should engage the stakeholders in news media. The quality and prestige of a democracy is influenced by the level of its press freedom.
Ringing Out The Old
New vehicle scrappage policy reflects awareness of pollution concerns. It’s also in sync with effort to reduce road accidents.
Editorial
Announcing the government’s new policy for scrapping old and unfit automobiles last week, Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari gave estimates of the country’s old car fleet. About 1 crore vehicles more than 15 years old ply on the country’s roads. Given the well-documented environmental and road safety risks of such large numbers of old automobiles, the policy is a step in the right direction. It frames a phased and non-coercive approach to flushing out polluting and unsafe vehicles. At the same time, it allows the minuscule number of owners of “sentimental” vehicles and collectors of unique automobiles to preserve them, albeit at a price. The policy will kick in from April 2022 with the government setting an example by retiring about 2.3 lakh old vehicles owned by various agencies under it. Mandatory tests for heavy commercial vehicles will begin from April 2023 and for other automobiles in June 2024. The policy aims to nudge vehicle owners into compliance through a system of incentives and disincentives. It is also expected to stimulate the auto industry and boost fuel-efficiency in the long run.
Diesel vehicles older than 10 years and petrol vehicles that have run more than 15 years are banned on Delhi’s roads following the NGT ruling of 2015. Two years ago, West Bengal initiated a scheme to phase out more than 15-year-old commercial vehicles — the plan has not yet come into effect, reportedly because of the COVID pandemic. The National Clear Air Programme of 2019 asks cities to frame policies to retire old cars but it does not define the criteria for end-of-life vehicles. The policy announced last week will provide a roadmap to these sporadic initiatives. In the coming months, however, the government will have to seek legal opinion to clear the air on whether the new policy will take precedence over the NGT ruling on Delhi.
The announcement of the scrapping policy coincided with the sobering conclusions of the World Air Quality Report: Twenty-two of the 30 most polluted cities in the world are in India — transportation is among the major sources of air pollution. The scrapping policy is a reassuring testament to the government’s awareness of such concerns. It’s also in sync with its endeavour to reduce road accidents by introducing safety provisions in the Motor Vehicles Act 2019. The policy will ensure that more cars on Indian roads are equipped with the rapidly improving technology to secure passengers during a crash. The government must now take the next step for modernising the country’s car fleet by introducing the long-awaited electric vehicle policy.
Corrective voice
The SC did well to lay down guidelines for the judiciary in dealing with cases of sexual crime
Editorial
While recognising society’s deep-rooted patriarchy and initiating a course correction in the way the judiciary itself views gender rights, the Supreme Court went back to Henrik Ibsen, a playwright known for his feisty women characters who break free of traditions of familial confines and notions of social propriety. Setting aside an absurd rakhi-for-bail order of the Madhya Pradesh High Court to a sexual offender, the Court issued a set of guidelines on March 18 to be followed by the judiciary while dealing with sexual crimes against women. The two-member Bench of Justices A.M. Khanwilkar and S. Ravindra Bhat used a quote from Ibsen to say that a woman ‘cannot be herself’ in an ‘exclusively masculine society, with laws framed by men’, and laid it down as a guiding force for all future judicial proclamations. The judiciary’s corrective voice is a welcome step in the aftermath of CJI S.A. Bobde’s reported remarks during a virtual hearing, when he asked an alleged rapist’s lawyer to find out whether his client would marry the victim. He later said he had been misquoted. The Khanwilkar-Bhat Bench asked all courts to refrain from imposing marriage or mandate any compromise between a sex offender and his victim. Powerful men seem to be reiterating misogyny besides carelessly linking sexual crimes to women being alone at night or wearing clothes of their choice.
Leaning on the ‘Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia’, the Bench listed a host of avoidable stereotypes: women are physically weak; men are the head of the household and must make all the decisions related to family; women should be submissive and obedient. Women are battling society’s ingrained prejudices, and the judgment acknowledges this bitter reality, saying gender violence is most often shrouded in a culture of silence. Pointing to the entrenched unequal power equations between men and women, including cultural and social norms, financial dependence, and poverty, it said data may not reflect the actual incidence of violence against women. It is not the first time the Supreme Court is clamping down against gender stereotyping. Justice D.Y. Chandrachud (Secr., Ministry of Defence vs. Babita Puniya) had argued against treating women in the Army any differently from their men counterparts for they worked as “equal citizens” in a common mission, and in Anuj Garg, the Court had called out the “notion of romantic paternalism” as an attempt to put women “in a cage”. To break the silence on bias against women, everyone must take responsibility, especially institutions and those in important positions. The Court’s reiteration on where it needs to stand on women’s rights is a move in the right direction because the fight for gender equality is far from over.
सिस्टम में खामी की सजा गरीबों को क्यों
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद उचित मुद्दे पर सरकार से अपनी नाराजगी व्यक्त की है। केंद्र ने संसद को फरवरी 2017 में बताया कि आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के बाद 3.95 करोड़ फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए गए। बाद में पता चला कि जिन गरीबों के कार्ड निरस्त हुए उनमें से अधिकांश मामलों में तकनीकी, प्रशासनिक व भ्रष्टाचार जनित अक्षमता एक बड़ा कारण था। कोर्ट का कहना है कि इन कमियों के कारण गरीबों का अनाज मिलने का अधिकार क्यों खत्म किया गया, जबकि जरूरत थी कमियों को दूर करने की। दरअसल जहां केंद्र ने आधार से लिंक न होने वाले राशन या अन्य पहचान पत्रों को फर्जी माना, वहीं राज्य सरकारों को इस मद में होने वाले खर्च में कटौती का मौका मिल गया। इससे भ्रष्ट अधिकारी-दुकानदार गठजोड़ को इसके नाम पर बेहद सस्ता राशन महंगा बेचने का धंधा शुरू करने का मौका भी मिल गया। गरीबों की शिकायत नक्कारखाने में तूती की आवाज बन कर रह गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के दो-तिहाई लोगों को पांच किलो अनाज प्रति माह एक से तीन रुपए की दर से मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने तीन साल पहले कहा था कि आधार का औचित्य कल्याणकारी योजनाओं को सही व तेजी से लागू करने में है। कोर्ट की नाराजगी है कि सिस्टम त्रुटिपूर्ण है तो सजा गरीबों को क्यों ?
Date:24-03-21
कोरोना से भारत में ही गरीबों की संख्या ज्यादा क्यों बड़ी
योगेंद्र यादव, ( सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इंडिया )
पिछले हफ्ते चौंकाने वाली खबर आई: कोरोना के धक्के से पूरी दुनिया में जितने लोग एक झटके में गरीब हो गए, उनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ भारत में थे। हमारे यहां लगभग साढ़े सात करोड़ लोग पिछले साल गरीबी की गर्त में धकेले गए। कोई और देश होता तो इस खबर पर बहस होती, सवाल पूछे जाते, सफाई दी जाती। लेकिन बलिहारी है मेरे देश की। यहां यह खबर सन्नाटे में डूब गई। बस एक-दो अखबारों ने इसपर ध्यान दिया।
एक टीवी चैनल ने इस पर चर्चा करने के लिए भी मुझे बुलाया लेकिन दस मिनट पहले विषय बदलकर मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख का सनसनीखेज पत्र करना पड़ा। मेरा भारत महान!
यह खबर एक अमेरिकी संस्था प्यू रिसर्च सेंटर की विश्वव्यापी रिपोर्ट से निकली थी। यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि रपट दुनियाभर के गरीबों के किसी नए सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है। इस रपट में दुनिया के तमाम देशों में आय के बंटवारे के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि कोरोना का उस देश के अलग-अलग वर्ग की आय पर क्या असर हुआ होगा। इस अनुमान का आधार है, हर देश की जीडीपी यानी राष्ट्रीय आय पर पिछले साल हुई कमी या बढ़ोतरी का आंकड़ा। वर्ष 2020 दुनियाभर की अर्थव्यवस्था के लिए खराब रहा। जहां हर साल राष्ट्रीय आय में कुछ न कुछ वृद्धि होती है, वहां पिछले साल अधिकांश देशों की राष्ट्रीय आय घटी। विश्व बैंक का अनुमान है पिछले वर्ष हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ने की बजाय लगभग 10% कम हो गई।
यह रपट राष्ट्रीय आय में हुई इस कमी का अलग-अलग वर्गों पर हुए असर का अनुमान लगाती है। रपट मानकर चलती है कि अगर पूरे देश की आय 10% कम हुई है, तो हर परिवार, हर व्यक्ति की आय भी 10% कम हुई होगी। लेकिन दुनिया का अनुभव बताता है कि सबसे गरीब वर्ग को सामान्य से ज्यादा धक्का पहुंचता है, अमीरों को तो संकट में भी मुनाफा होता है। पिछले दिनों खबर आई कि पिछले साल गौतम अदाणी की आय और संपत्ति दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ी है। इसलिए कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि गरीबों की स्थिति इस रपट में बताई गई स्थिति से भी ज्यादा बुरी है।
फिलहाल इस रपट को मानकर चलें। इस विश्लेषण के अनुसार पिछले साल पूरी दुनिया में लगभग 13 करोड़ मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग गिरकर गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए। (यह रपट प्रतिदिन 2 डॉलर यानी ₹145 से कम पर गुजारा करने वाले को गरीब परिभाषित करती है) इसमें से लगभग 7.50 करोड़ सिर्फ भारत से थे। पूरी दुनिया की आबादी में भारत का हिस्सा लगभग 18% है। लेकिन पिछले साल गरीबी के गर्त में गिरने वालों में 57% भारत से थे। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ख्वाब देखने वाले और कोरोना से प्रभावी तरीके से निपटने का दावा करने वाले देश के लिए यह आंकड़ा बड़े सवाल खड़े करता है।
इसी असर को दूसरे छोर से भी देखा जा सकता है। इस रपट के मुताबिक पिछले साल भारत के मध्यम और ऊपरी वर्ग की संख्या में बहुत भारी गिरावट आई है। लॉक डाउन से पहले हमारे देश लगभग 12.5 करोड़ लोग ऐसे परिवार में रहते थे जिसे संपन्न परिवार कह सकते हैं, जिस परिवार की मासिक आय एक लाख रु. से अधिक है। पिछले वर्ष में यह संख्या घटकर 8.5 करोड़ हो गई। यानी एक साल में ही मध्यम या उच्च वर्ग की जनसंख्या चार करोड़ घट गई। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि वर्ष 2020 ने पिछले 20 वर्ष की आर्थिक वृद्धि के फायदे को एक ही झटके में खत्म कर दिया और देश को वापस वहां खड़ा कर दिया जहां वह इस शताब्दी के आरंभ में था।
उम्मीद करनी चाहिए कि मीडिया में न सही, अर्थशास्त्रियों में इस रिपोर्ट को लेकर गंभीर बहस होगी। बेशक अर्थशास्त्री इस रपट को अंतिम सत्य न मानकर राष्ट्रीय आय के किसी जमीनी सर्वेक्षण का इंतजार करेंगे। अफसोस की बात है कि वर्ष 2011 के बाद से राष्ट्रीय सैंपल सर्वे की मासिक आय व्यय सर्वेक्षण की रपट सार्वजनिक नहीं हुई है। एक सर्वेक्षण हुआ, लेकिन उसकी रिपोर्ट तकलीफदेह थी इसलिए रपट को मोदी सरकार ने कूड़ेदान में डलवा दिया। जब कभी राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण पूरा सच देश के सामने लाएगा, तो सच इस रपट से भी खौफनाक निकलेगा।
पिछले साल जब पूरे देश ने प्रवासी मजदूरों के पलायन के दृश्य देखे थे, तब यह सवाल उठा था कि भारत से ज्यादा गरीब अफ्रीका के देशों से भी ऐसी हृदय विदारक तस्वीरें देखने को क्यों नहीं मिलीं? प्यू रिसर्च सेंटर की नवीनतम रपट हमें दोबारा ऐसे ही कड़े सवाल पूछने पर मजबूर करती है: कोरोना वायरस का आर्थिक धक्का पूरी दुनिया में सबसे अधिक भारत पर ही क्यों पड़ा? क्या महामारी का प्रकोप भारत में बाकी दुनिया से ज्यादा था? या भारत में जिस तरह बिना तैयारी और बेरहमी से लॉकडाउन किया गया, वह इस धक्के के लिए जिम्मेदार है? देश की हर छोटी बड़ी उपलब्धि के लिए श्रेय लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कड़े प्रश्न से पल्ला नहीं झाड़ सकते।
Date:24-03-21
जीवन की सारी जरूरतें अंतत : वनों से जुड़ी है
डॉ अनिल प्रकाश जोशी, ( पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक )
21 मार्च वन दिवस तो गुजर गया, मगर यह सिर्फ रस्म अदायगी भर न रह जाए। इस बार की थीम फॉरेस्ट रेस्टोरेशन मतलब इनके संरक्षण से जुड़ी है। इसमें साफ है कि ये प्राकृतिक वनों के विस्तार व उनकी बहाली से संदर्भित है। ये बिलकुल सच भी है, आज अगर दुनिया में वनों को लेकर कोई बड़ी चिंता है तो वो प्राकृतिक वनों के संरक्षण की है। खासतौर से तब, जब प्रति वर्ष 100 लाख हेक्टेयर वन खत्म हो रहे हों और प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्र घट रहा हो। पर शायद सबसे पहले हमें वनों के महत्व को नए सिरे से सबके सामने रखना और सबको इस तथ्य से जोड़ना होगा कि वन विहीनता, हमें जीवन विहीन कर देगा। जीवन की कोई भी आवश्यकता ऐसी नहीं है जो अंततः वनों से न जुड़ी हो।
वन भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं। पर दुर्भाग्य है कि हमारे देश में वनों के हालात बेहतर नहीं कहे जा सकते। साल 1980 में सरकारों ने गंभीरता दिखाते हुए एक वन नीति को लाने की कोशिश की, जिसके अनुसार किसी भी राज्य और देश में 33 फीसदी वनभूमि होनी चाहिए। पर एकाध राज्य ही है, जहां 33 फीसदी वनों का दावा किया जा सकता है। हरियाणा-पंजाब जैसे हरित क्रांति के राज्य वन विहीन हैं। उत्तरप्रदेश में यह 4-5% ही है, बिहार में 7, पश्चिम बंगाल में 14 फीसदी। यह आंकड़ा अपेक्षित क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है। हां हिमालयी राज्य उत्तराखंड और मध्यप्रदेश व झारखंड जैसे राज्य निश्चित रूप से वनाच्छादित हैं और यही कारण है कि देश में आज लगभग 21.6 फीसदी भूमि में वन पाए जाते हैं।
एक बड़ा पहलू वनों की स्थिति को लेकर भी है। क्या यह बेहतर वन के दर्जे में आते हैं? वनों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी दशा कैसी है और साथ में किस प्रजाति की भागीदारी ज्यादा है। अगर वन प्रजातियां पारिस्थितिकी दृष्टि के अनुरूप नहीं है तो निश्चित रूप से वह बेहतर नहीं कहे जा सकते। उदाहरण के लिए हिमालयी क्षेत्रों में चीड़ के वन, बेहतर वन की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि इनका पारिस्थितिकी योगदान उस दर्जे का नहीं है, जो कि हिमालय के लिए अपेक्षित है। हां, आर्थिक दृष्टिकोण से जरूर महत्व हो सकता है, क्योंकि यह लीसा (रेजिन) के रूप में ज्यादा जाना जाता है। अगर सवाल पारिस्थितिकी और पर्यावरण का है, तो वृक्षों की प्रजाति, जो क्षेत्र विशेष के साथ जुड़ी है उसका योगदान ज्यादा महत्वपूर्ण है न कि मात्र वृक्ष का। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर हिमालय क्षेत्र में सागौन या यूकेलिप्टस की बहुतायत हो तो वह अच्छे वन क्षेत्र तो बन सकते हैं पर बेहतर वन की श्रेणी में नहीं आएंगे। और ऐसा उन सभी प्रजातियों के लिए समझना जरूरी है जिनका पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से कोई योगदान ना हो।
शास्त्रों में कहा गया है कि एक वृक्ष सौ पुत्र समान, मतलब 100 पुत्र उतनी सेवा नहीं करते जितना कि मात्र एक वृक्ष करता है और यह सही भी है। एक वृक्ष एक किमी तक शुद्ध प्राणवायु फैला सकता है। दुनिया की इस बढ़ती आबादी के लिए हमें आज एक हजार अरब वृक्ष चाहिए जो करीब 810 अरब टन कार्बन डाइ-ऑक्साइड को शोषित कर सकें।
वर्ष 1990 से 2015 के बीच में वन संसाधन आकलन के अध्ययन की सितंबर 2015 में आई रपट के अनुसार दुनिया में वन 31.6 फीसदी से घटकर 30 फीसदी पर पहुंचे हैं। हां इसके बाद वनों में बढ़ोतरी हुई है पर यह समान रूप से नहीं रही है। एक और अध्ययन में सामने आया कि दुनिया में तीन चौथाई इलाकों में बेहतर पानी का कारण वहां के बेहतर वन ही रहे। दुनिया में जो बड़े 230 जलागम हैं, उनमें 40 फीसदी जलागमों में 50% तक वनों की क्षति हुई है और अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले समय में हमें भीषणजल संकट का सामना करना पड़ेगा। हमें यह भी समझ लेना चाहिए की यह वन ही हैं जो बढ़ते जलवायु परिवर्तन को हमारे हित में साध सकते हैं।
 Date:24-03-21
Date:24-03-21
संयुक्त राष्ट्र आयोग के प्रस्ताव के बाद भांग की बढ़ सकती है मांग
सुरिंदर सूद
मादक पदार्थों पर गठित संयुक्त राष्ट्र आयोग ने दिसंबर में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कैनबिस यानी भांग को सर्वाधिक खतरनाक मादक पदार्थों की श्रेणी से हटा दिया गया। इसके बाद इस बहुपयोगी पौधे के लिए अपना खोया हुआ रुतबा हासिल करने का रास्ता साफ हो गया है। यह किसानों के लिए लाभदायक फसल होने के साथ ही प्रसंस्करण उद्योग के लिए कीमती कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था जहां मौज-मस्ती, खाने और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भांग उगाने और उसके सेवन का इतिहास रहा है। इसे धार्मिक मान्यता के साथ मादक पदार्थों की तुलना में कम नुकसानदायक नशे के तौर पर सामाजिक स्वीकृति भी मिली हुई है। कोकीन की तुलना में तो यह बहुत कम नुकसानदायक है।
फिर भी अमेरिका जैसे कुछ देशों के दबाव में भांग के उत्पादन पर रोक लगी हुई थी। भारतीय मादक पदार्थ एवं मानसिक उद्दीपक तत्त्व (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत इसे 1985 में प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में रख दिया गया था। संशोधन के बाद राज्य सरकारों को मौज-मस्ती से इतर मकसद से भांग की नियंत्रित एवं विनियमित खेती की मंजूरी देने का अधिकार दे दिया गया था लेकिन तमाम राज्यों ने ऐसा नहीं किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र ने भांग को हेरोइन एवं कोकीन जैसे अधिक नुकसानदायक एवं लत लगाने वाले पदार्थों से अलग कर दिया है। इस कदम ने भांग के औषधीय गुणों, औद्योगिक स्तर एवं खानपान में इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। यह बदलाव भांग की खेती, अपने पास रखने, खरीद-बिक्री करने और मूल्य-संवद्र्धन को खुद ही अपराध-मुक्त कर देता है। भांग रखने के आरोपों के आधार पर प्रताड़ित या दंडित करने की आशंका भी कम हो गई है। हाल ही में हम एक बॉलीवुड अभिनेता की रहस्यमयी मौत के मामले में ऐसे आरोप देख चुके हैं। अब केंद्र को स्थानीय मादक पदार्थ अधिनियम पर ध्यान देकर उसका संशोधन करने की जरूरत है ताकि भांग के बारे में संयुक्त राष्ट्र संस्था के रुख में आए बदलाव को रेखांकित किया जा सके।
खासकर, भांग उत्पादकों एवं संभावित निवेशकों ने घरेलू एवं निर्यात बाजारों के क्षेत्र में विशाल अवसर की तलाश शुरू कर दी है। एक अमेरिकी सलाहकार फर्म के मुताबिक भांग का वैध बाजार वर्ष 2027 तक 3.6 अरब डॉलर हो सकता है जो 18 फीसदी से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान भारत में भांग पर आधारित आयुर्वेदिक एवं चिकित्सकीय उत्पादों का बाजार भी बढ़कर 12-14 करोड़ डॉलर हो जाने का अनुमान है। हाल में कई स्टार्टअप एवं छोटी औद्योगिक इकाइयां इस संभावना के दोहन के लिए सामने आ चुकी हैं।
भारतीय भांग (कैनबिस इंडिका) और उसके यूरोपीय संस्करण हेम्प (कैनबिस सतिवा) मोटे तौर पर एक जैसे ही गुण रखते हैं लेकिन उनके रासायनिक संयोजन एवं उपयोग में हल्का अंतर होता है। इन दोनों ही किस्मों के पौधों में कीमती रेशा एवं बीज होते हैं लेकिन कैनबिस इंडिका दो अहम मादक तत्त्वों कैनबिनॉयड के मामले में अधिक समृद्ध है। टेट्रा-हाइड्रो-कैनबिनॉल (टीसीएच) के नाम से चर्चित पहला तत्त्व बुनियादी मनो-सक्रिय पदार्थ है जो उसका सेवन करने वाले को ‘ऊंचा उड़ने’ का अहसास दिलाता है। कैनबिडॉयल (सीबीडी) कहा जाने वाला दूसरा तत्त्व कम उद्दीपक होता है और अपने उपचारीय गुणों की वजह से दवाओं में उसका खूब इस्तेमाल होता है।
भांग की पत्तियों एवं फूलों को सूखाकर तैयार किया गया चूर्ण भारत में चरस, गांजा और भांग के नाम से जाने जाते हैं जबकि दूसरे देशों में इसे मारियुआना, वीड, पॉट या डोप का नाम दिया जाता है। असल में, चरस और गांजे का इस्तेमाल एक लोकप्रिय पेय ‘भांग’ बनाने में भी अक्सर होता है। ताजी पत्तियों एवं फूलों को मसलने से निकला रेसिन हशीश कहा जाता है। इन पौधों के तने में मौजूद रेशों का इस्तेमाल ग्रामीण कलाकार रस्सियां बनाने एवं कुछ उपयोगी हस्तशिल्प उत्पाद तैयार करने में भी करते हैं।
भांग के पौधे के उपचारात्मक मूल्य को दर्शाने वाले साहित्य से पता चलता है कि यह ग्लूकोमा का इलाज कर सकता है, शरीर के अन्य हिस्सों में कैंसर का फैलाव रोक सकता है, अल्जाइमर रोग के बढ़ने की रफ्तार धीमी करने में मददगार है। इसके अलावा यह तनाव कम करने और भोजन को ऊर्जा में तब्दील करने के लिए उपापचय तेज करने में भी मददगार माना गया है। कुछ अध्ययन दिमाग की रचनात्मक क्षमता में सुधार से भी इसका ताल्लुक जोड़ते हैं।
भांग के उम्दा किस्म के उत्पादों के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश इस औषधि की आर्थिक क्षमताओं के दोहन के लिए किसानों एवं उद्यमियों की मदद करने को आगे आया है। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 11 मार्च को बजट भाषण में कहा कि भांग की नियंत्रित खेती को जल्द ही कानूनी बनाया जाएगा। कुल्लू जिले में स्थित मलाणा घाटी हशीश की खास किस्म के लिए दुनिया भर में मशहूर है। भांग की पत्तियों को हाथों के बीच रगड़कर यह रेसिन तैयार की जाती है। भारत के भीतर और बाहर इसके ऊंचे दाम मिलते हैं। मलाणा रेसिन के उत्पादक इसके लिए भौगोलिक सूचक (जीआई) निशान दिए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन इसकी संभावना कम ही है कि ऐसे उत्प्रेरकों की पैदावार को सरकारी नीति के तौर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने का मतलब यह भी होगा कि मौज-मस्ती से इतर कामों में इस पौधे के वाणिज्यिक इस्तेमाल को बढ़ावा मिले।
बहरहाल हिमाचल प्रदेश दूसरे राज्यों के लिए एक नजीर पेश कर रहा है। केंद्र सरकार को भी भांग के पुनर्वास के लिए एक अनुकूल कानूनी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। ऐसा होने पर ही भांग किसानों के लिए कमाऊ फसल, शिल्पकारों एवं उद्यमियों के लिए कीमती कच्चे माल और सरकार के लिए राजस्व का स्रोत बन पाएगा।
महिला सुरक्षा का संकट
बिभा त्रिपाठी
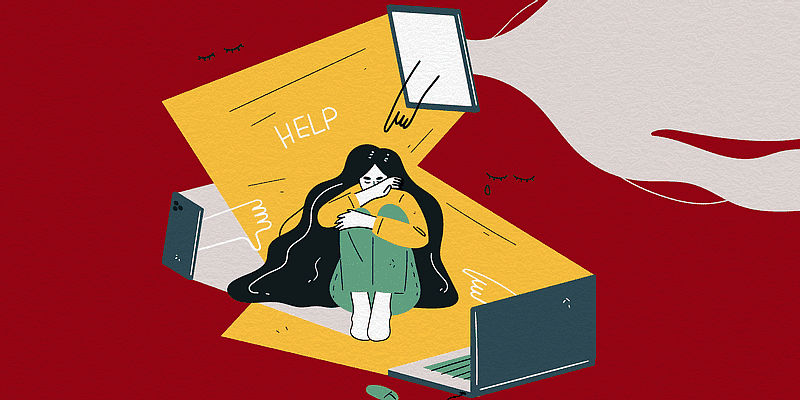
इस आंदोलन की मुख्य बात यह है कि इसमें हुए अध्ययन यह दर्शाते हैं कि लैंगिक विषमता को खत्म करने के लिए अभी दो सौ सत्तावन साल और लगेंगे और ऐसे आंदोलनों का आधार स्तंभ यह सूत्र वाक्य होता है कि ऐसे पुरुष, जो शक्ति और अधिकार संपन्न हैं, उन्हें महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस बात में कतई संदेह नहीं है कि जहां महिलाओं ने पुरुषों का साथ और सहयोग पाया है वहां वह और सशक्त होकर उभरी है, अपनी क्षमताओं को और भी निखारा है और अपने अपने क्षेत्रों में परचम भी लहराया है, परंतु जिस आंदोलन के सूत्रधार ही अभी पूर्ण समानता आने में ढाई सदी से अधिक का समय देते हैं! वहां एक सरल और साधारण प्रश्न यह उठता है कि क्या आज की परिस्थितियों पर हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें और मूकदर्शक बन कर देखें कि महिला का शीलभंग हो रहा है, गलियों में, चौराहों पर, घरों की चारदीवारी के भीतर, सुधार गृहों में, आश्रमों में, अनाथालयों में और आश्चर्यजनक रूप से पुलिस थानों में भी। यह ऐसी जगह है, जहां किसी महिला को सर्वाधिक सुरक्षा का अहसास होना चाहिए। और जब इन जगहों पर भी उसे खौफनाक मंजर दिखाई देते हैं तो प्रश्न उठता है व्यवस्था पर, राजनीति पर, शासन पर और प्रशासन पर। जिस देश का नेतृत्व संभालने वालों को अपराधों के घटने का क्रम उसकी गंभीरता और निरंतरता किसी राज्य विशेष के राजनीतिक दल के संदर्भ में व्याख्यायित करना हो वहां एक उदासी, छलावा और निराशा के अलावा कुछ नहीं बचतो
अब हमें यह समझना होगा कि महिला हिंसा की कोई जाति नहीं होती, कोई नस्ल नहीं होता, कोई धर्म, मजहब भाषा या क्षेत्रीयता नहीं होती। महिलाओं को धन, धर्म और वर्ग में विभाजित करके हम उन्हें कोई न्याय नहीं दे पाते। दुखद यह है कि दलित, आदिवासी, घरेलू कामों को करने वाली या कामकाजी महिलाओं के भीतर जो सुरक्षा का भाव स्वाधीनता के सत्तर साल बीतने के बाद आ जाना चाहिए था, वह अब भी संभव नहीं हो पाया है। विडंबना तो यह है कि उच्च पदस्थ महिलाओं को, जिनमें कुछ सेना में तो कुछ पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, उन्हें भी यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, उनके ऊपर भी अपनी आवाज को दबाए रखने का दबाव पड़ रहा है।
ये परिस्थितियां देश के स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं है। सरकारी नीतियों, नियमों, कानूनों, योजनाओं और घोषणाओं का दायरा बड़ा सीमित होता है, इसके लाभार्थियों की सोच और प्रयास आत्मकेंद्रित होती है, इसमें महिला पुरुष का तथाकथित विभाजन भी महत्त्वहीन हो जाता है।
आपराधिक न्याय प्रशासन के सभी अंगों के सक्रिय और संवेदनशील होने के बावजूद पीड़ित पक्षकार के न्याय का रास्ता दुरूह और दुर्गम बना हुआ है। निर्भया कांड के बाद किए गए बदलाव और एक कॉरपस निधि बनाए जाने के बावजूद शून्यता व्याप्त है। जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पर समय पर काम नहीं करते और खेतों खलिहान में दिन में या रात में घटने वाली घटनाओं में कोई फर्क नहीं होता। हमारे देश में राष्ट्रीय अपराधों की सांख्यिकी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नामक संस्था द्वारा तैयार होती है, जो उन पीड़ितों का हवाला नहीं देती, जिन्होंने आपराधिक न्याय प्रशासन को अपनी ओर से गतिमान नहीं किया है, चाहे वह वयस्क अपराध पीड़िताएं हों या अवयस्क पीड़िताएं।
ऐसे में जहां विश्व के अन्य देशों में राष्ट्रीय अपराध पीड़िता सर्वेक्षण या राष्ट्रीय अपराध पीड़ित ब्यूरो जैसी संस्थाएं स्थापित की गई हैं और जिनके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है, जो किसी न किसी प्रकार के हिंसा, उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, शोषण अथवा विभेद के शिकार हो रहे हैं, ताकि उनके लिए नीतियां बने और उन्हें उनके घर, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थल, मल्टीप्लेक्स, लिफ्ट, अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर, बाथरूम आदि जगहों पर भी सुरक्षित रखा जा सके। वास्तव में देश की बात करें या वैश्विक परिदृश्य की चर्चा करें, एक समाज के विचलन के अनेक केंद्र होते हैं। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, फिल्में और अब वेब सीरीज के माध्यम से जिस समाज का चित्रण किया जा रहा है वह ऐसा समाज है जिसका कोई मानक नहीं है, जिसमें कोई प्रतिमान नहीं है, जिसमें नैतिकता की कोई भूमिका नहीं है, जिसमें नशा, लैंगिक दुराचरण, अश्लीलता और आपराधिकता में कुछ भी असहज या अस्वाभाविक नहीं समझा जाता और सब कुछ ऐसे परोसा जाता है जैसे यही नया रिवाज हो। सूचना क्रांति एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति के दुरुपयोग ने रिश्तों की मर्यादा को भी तार-तार कर दिया है, प्रख्यात मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड के शब्दों में कहा जाए तो पूरे के पूरे जनमानस का सुपर ईगो जिसे मर्यादा और आदर्शों का पुंज कहा जाता था, एक विलुप्त होती प्रजाति के समान विलुप्त होता दिखाई दे रहा है, सभी के भीतर का ईगो उसे नियंत्रित कर रहा है, उनका चेतन मन जिसे अहं या ईगो की संज्ञा दी जाती है, वह बिल्कुल निस्तेज हो चुका है और ईडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा काम्प्लेक्स जो क्रमश: पिता और पुत्र के बीच तथा माता और पुत्री के बीच होता है, उसने हर उम्र के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है।
एक तरफ द्रुत गति से हो रहे बदलावों के मद्देनजर हमारी न्यायपालिका लैंगिक रूप से अनुमन्य समाज का गठन कर रही है, जहां विवाह और परिवार जैसी संस्था से लोग पल्ला झाड़ रहे हैं और आधुनिकता के नाम पर हावी होती नग्नता के शिकार हो रहे हैं, वहां यह भी उल्लेखनीय है कि एक तरफ जो लड़का, युवा या प्रौढ़ स्वयं को आधुनिकता का पोषक मानता है, व्यक्तित्व के अनछुए हिस्सों में रूढ़िवादी पितृसत्ता का वर्चस्व भी बनाए रखता है। व्यक्तित्व के इस दोहरेपन की मार उन तथाकथित आधुनिक, शिक्षित और पेशेवर महिलाओं को ज्यादा झेलनी पड़ती है, जिन्होंने सोचा था कि उनकी मांओं का उत्पीड़न विवाह संस्था में बंधने के कारण होता है और इसलिए उन्होंने एक विरोध का बिगुल बजाया और स्वच्छंदता की राह पकड़ी।
कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमारा समाज, जिसमें पुरुष एवं महिला और उभय लिंगी सभी शामिल हैं, उसमें श्रम और शरीर का सम्मान करना नहीं सिखाया जाएगा तब तक महिला सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिल पाएगा। वर्तमान समय में ‘ही फार शी’ या ‘मेन फॉर विमेन’ के साथ ही ‘शी फार ही’ और ‘शी फार शी, विमेन फॉर मेन’ और ‘विमेन फॉर विमेन’ की भी बात करनी होगी। किसी व्यक्तिगत पहलू का सामान्यीकरण करना विषय की गंभीरता को कमतर करना होता है, अत: घटनाओं का निरपेक्ष विवेचन करना चाहिए, उनका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और एक नई मुहिम ‘समाज बदलाव के लिए’ ‘सोसायटी फॉर चेंज’ ‘एस फॉर सी’ चलाना चाहिए, जिसमें ‘सब सब के लिए’ ‘ऑल फार आल’ या ‘ए फॉर ए’ के लिए काम करें तो शायद हम अपने समाज की सुरक्षा के लिए आश्वस्त हो सकें।
दिल्ली की नई आबकारी नीति
संपादकीय

