
25-03-2021 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:25-03-21
Date:25-03-21
Indefensible Quotas
Breaching the 50% reservation ceiling is harmful. It will ghettoise India
TOI Editorials
India’s founding fathers opted to have a simple standard to define the fundamental right to equality. The Constitution didn’t provide for special dispensations. This state of affairs didn’t last long. Among the first constitutional amendments was one that created a special dispensation for socially and educationally backward classes, to provide for reservation in education and jobs. Since then the ambit of reservation has steadily expanded. A Supreme Court bench is once again hearing a similar case.
A five-judge constitution bench is weighing arguments in a case where Maharashtra expanded the reservation limit for socially and educationally backward groups beyond 50% by creating a special dispensation for the Maratha community. The 50% ceiling has largely been the rule for almost six decades. The underlying logic is that this is already an extremely high ceiling for special dispensations; expanding them further can only be at the cost of merit and the right to equality. The Maratha reservation case assumes salience because not only have many states supported the breach of 50% cap, even the Centre has backed it. Simply put, there’s consensus among political parties that a majority of seats and government jobs should be given on the basis of identity. SC must resist this populist push and stand up for constitutional values.
The 50% cap was breached a couple of years ago when an amendment was passed providing additional 10% reservation for economically weaker sections. This amendment has been challenged and another SC bench will hear the case. The constant expansion of the reserved pie is indefensible. Increasingly, socially dominant groups have agitated for inclusion in reserved categories. Reservation has become a substitute for seven decades of underperformance in providing quality education to all. This approach is short-sighted.
Expanding reservations have only led to a hardening of narrow group identities. Electoral power politics has often led to numerically dominant groups gaining at the expense of others in the reservation sweepstakes. Another fallout is the discouragement of individual initiative. Group identity is becoming more important than an individual’s pursuit of excellence in deciding career trajectories. India’s reservation policy no longer adheres to the spirit of the fundamental right to equality, as it exists in the Constitution. If political parties are too craven to halt this populist lurch, it behoves SC to provide them some cover and uphold the Constitution’s spirit.
Date:25-03-21
Hurdles again
One step forward, two backward sums up India’s sporadic trysts with transgenic crop trials
TOI Editorials
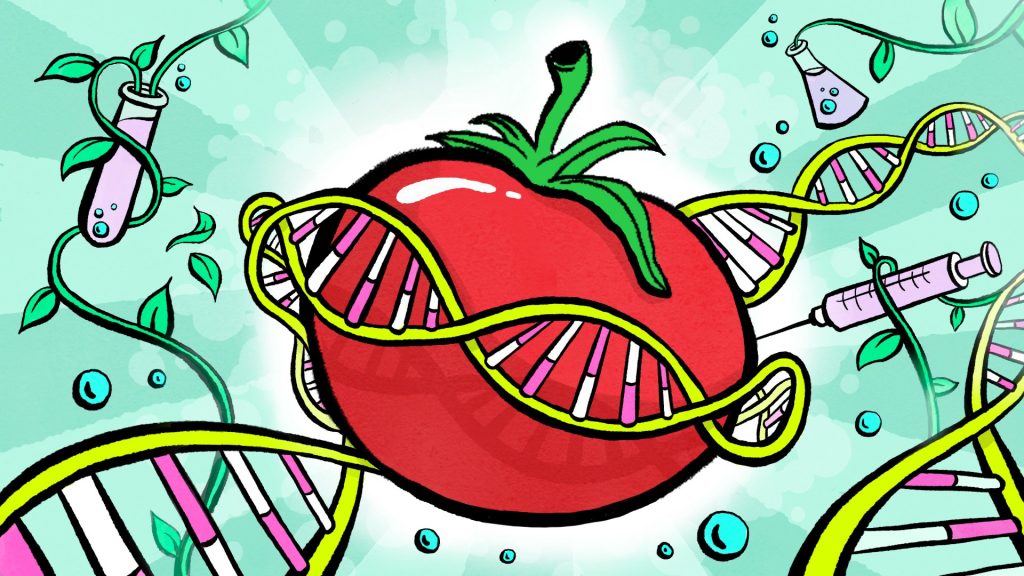
In deciding to consider proposals for GM crop field trials only upon the recommendation of state governments, Centre has signalled a retreat in another arena of farm reforms. Last year, central regulator Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) allowed biosafety field trials of two new transgenic Bt Brinjal varieties in eight states. RSS-affiliated Bharatiya Kisan Sangh asked the Centre and these states to deny no-objection certificates for the field trials. GEAC’s decision to initiate trials, a compulsory prelude to commercial release, was a completely scientific decision based on long-term ICAR studies.
Unfortunately the dogmatic opposition to transgenic crops rejects such findings, nor do they appreciate that the two Bt Brinjal varieties were developed indigenously. Field trials will help governments, scientists, seed companies and farmers transparently assess the claims of transgenic crops repelling pests and boosting productivity. Domestic research, indigenisation and Atmanirbhar Bharat are losing out. When circumstances force India to adopt GM crops in future, foreign biotech companies that have powered ahead during these two decades of domestic confusion will reap the advantages. Dangerous trends like farmers growing unapproved transgenic varieties of cotton and brinjal were reported amid stalling of trials.
For all the rhetoric on doubling farm incomes, Centre’s inability to overcome resistance to farm reforms is worrying. With the three farm laws earning the ire of Punjab, Haryana and western UP farm unions, BJP has toed the BKS’s line. Unelected lobbies have scored again, akin to the hyperactivism that influenced UPA’s flip-flops and slowing growth. Absent central push, states with far less heft are unlikely to promote transgenic crop trials. 42% of the Indian workforce is employed in agriculture, mainly at subsistence incomes. India will pay a heavy price for the populism in their name that chokes reforms to infuse technology, capital and private trade in agriculture. They deserve a better deal.
Roadworthiness, not vintage, for scrapping
ET Editorial
The Centre’s new motor vehicle scrappage policy can be sensible, provided it is implemented right. Older vehicles contribute disproportionately to tailpipe emissions and guzzle fuel. Recycling unfit, road-unworthy vehicles would have considerable economic benefits, too, provided the import duty on steel scrap is kept at the same level as on steel, to allow a domestic scrap industry to develop.
The policy calls for mandatory road fitness tests for commercial vehicles that are 15 years old. For other vehicles, the timeline is 20 years. Re-registration would now be a requirement for older vehicles. The way ahead, surely, is to incentivise regular testing and engine maintenance to purposefully stem pollution levels.
Vehicles need to be scrapped based on their road-fitness and not merely on vintage. A recent study did find that a well-designed scrappage policy can take a significant proportion of Bharat Stage 2 and 3 vehicles off the roads: nine million vehicles by 2022, and 28 million by 2025.
And it can rationalise fuel consumption by over nine million tonnes annually, bring down carbon dioxide emissions by 17% and that of particulate matter by 24%. There would be considerable benefits in organised recycling of steel, aluminium, plastics and rubber too.
Norms for testing and attendant infrastructure would be formalised by October, regular testing of heavy vehicles would begin by April 2023, and for other vehicles by June 2024. High fuel prices goad owners to opt for fuel-efficient vehicles.
Road tax concessions can, perhaps, be accorded depending on fuel efficiency. However, the peak GST rate of 28% on vehicles does need to be rationalised to step up much-needed efficiency in transport as the Indian economy picks up speed.
The Delhi arena
Governing Delhi requires will to uphold Constitution — not alter it
Shailaja Chandra

On the face of it, the amendment to the National Capital Territory Act 1991 was introduced in Parliament to give effect to a July 2018 judgement of a 5-judge constitutional bench. While purporting to do so, the Bill has, in fact, planted several curbs on the functioning of the legislative assembly of Delhi as well as its council of ministers. The Supreme Court, without striking one single note of dissent or dissonance in a 536-page order, clause by clause, had clarified the difference between the constitutional arrangement designed for Delhi and that available for any other Union Territory.
It had dwelt in detail with each aspect of the 69th Constitutional Amendment passed in 1991 through which Article 239 AA was added to the Constitution. The amendment envisioned a representative form of government for the NCT of Delhi which until then was just known as Delhi administration, with officers reporting directly to the lieutenant governor (LG). There were no ministers and scant public interface.
It was only after the 1991 constitutional amendment was passed that Parliament enacted the NCT of Delhi Act 1991 based on the constitutional mandate. It is to Clause 2 of Article 239 AA that the Supreme Court accords overriding primacy. Because it is there that the Constitution refers to an obligation (the word is shall) to establish a legislative assembly, with elected representatives on par with the legislatures of states. This is dissimilar to Article 239 B of the Constitution where Parliament has the discretion whether or not to create a legislature. The constitutional amendment also provided for Delhi’s legislative assembly to have the power to pass legislation on all subjects on the State and Concurrent lists of the Constitution, except for three — police, public order and land.
These three subjects remained under the Centre, to be administered by the LG of Delhi, and barring a case of difference of opinion arising between the LG and the council of ministers, the Constitution enjoined the LG to act on the “aid and advice” of the ministers. It went on to say that the “LG has not been entrusted with any independent decision-making power. He has to either act on the aid and advice or is bound to act on the order of the President if a matter is referred to him” (by LG). And that, observed the Supreme Court, should be the exception not the rule. The principle of collaborative federalism and constitutional balance must be exercised with “profound sagacity and judiciousness,” it added.
Leaving aside the Constitution and the Supreme Court, let us consider the ground realities based on first-hand knowledge of working in the erstwhile Delhi administration and later the Government of NCT (GNCT) of Delhi. In these times of intense polarisation, one cannot but marvel at the enormous reforms so successfully legislated and executed in the past.
Some landmarks which are remembered and enjoyed by the citizens include the privatisation of power by unbundling the Delhi Vidyut Board, the flagging off of Delhi Metro — the latter has remained a lasting partnership between the central and Delhi governments — the conversion of the largest fleet of public transport in the world to CNG, all of which happened in 2002. The unit area method of property tax collection was brought in by amending the Municipal Corporation Act 1956, giving enormous relief to harassed house owners. The Delhi Cooperative Societies Act 2003 brought fresh air into the murky functioning of cooperative societies. All these required the full backing and support of the then NDA government at the Centre and at least five central ministries. It was possible because there was a shared vision for Delhi, civility and respect for the observance of due process.
Ever earlier, several pathbreaking bills had been passed by the Delhi government on the floor of the Delhi assembly — notable being the Delhi Prohibition of Smoking Act and Non-Smokers Health Protection Act 1996, a first for the whole country — followed by a slew of bills for the Medical Council, Nursing Council and several other bodies.
The Supreme Court has referred to “skirmishes” between the two levels of government in its 2018 order and castigated “anarchy”. The reported nocturnal attack on the chief secretary at the official residence of the chief minister, the nine-day sit-in at Raj Niwas, the insistence on the acceptance of the Jan Lokpal Bill and the demand for statehood for Delhi, besides starting anti-corruption cases against people who were not even under the government, were incompatible with the constitutional scheme envisioned for Delhi. The citizenry was lulled into believing that a huge mandate implied possessing the power to do anything. To ensure that none of this happens again may have, at least partially, propelled the effort to clip the wings of the Delhi Government through the amendment to the NCT Act 1991.
Be that as it may, the amendment contradicts the inherent right of the legislature to frame rules for the conduct of its own proceedings. It also requires the government to obtain the LG’s opinion on decisions before executive action is taken, which runs counter to the constitutional bench’s specific interpretation on the need to inform but not to have to wait for a return of the LG’s opinion — something which could take days, or never come.
Once the amendment to the NCT Act is enacted, the Transaction of Business Rules 1993, which stipulates the procedure to be followed by the lieutenant governor and the council of ministers, will also need to be altered. Both remain subservient to the language of the Constitution.
Bharat ki rajdhani, India’s capital, needs a shared vision, maturity and the will to uphold the Constitution — not to alter it. It remains to be seen whether the legislation will hold up to the judicial review that is bound to follow.
Date:25-03-21
No case for selling public assets
Prabhaat Patnaik, [ Former professor of economics JNU ]
The government has adduced no reasons for the proposed privatisation of several public sector assets other than to generate resources for its spending. Let us see what such a fiscal strategy involves.
Nobody buys public sector assets by skimping on consumption. Nor does one buy such assets by skimping on investment: Current investment expenditure depends on decisions taken in the past and is more or less pre-determined. It is only investment decisions that are taken today for fructification tomorrow that may be scaled down by such a purchase; and if investment decisions taken today are scaled-down, then it is an authentic case of “crowding out” and such a strategy should be avoided anyway.
Selling public sector assets therefore does not “release” any resources from private use for government spending. The resources the government obtains by spending the sale proceeds of public assets are none other than the resources lying idle in the economy. Output that could have been produced by utilising idle capacity and unemployed labour, but is not produced because of lack of demand, now gets produced as demand gets generated by government spending financed by the sale of public assets. One can visualise the entire process as follows. The government borrows say Rs 100 from banks, uses it for spending, and then sells public assets worth Rs 100 to raise this money and return it to the banks, so that its net indebtedness does not go up.
It follows that financing government spending by selling public sector assets is basically no different from a fiscal deficit. In the latter case, the government puts its bonds — directly, or indirectly via banks — in private hands; in the former case, the government puts its equity (held in public sector assets) in private hands. The only difference between a fiscal deficit and selling public assets lies in the nature of the government paper that is handed to the private sector, but the macroeconomic consequences of a fiscal deficit on the economy are no different from those of selling public assets. Finance capital, and institutions like the IMF, do not recognise this fact, and treat the sale of public assets on a different footing from a fiscal deficit, for ideological — not economic — reasons, because they ideologically favour a dismantling of the public sector.
What, it may be asked, is wrong with a fiscal deficit? Not what is commonly suggested. In a situation of demand-constraints, where unutilised capacity and unemployed workers exist aplenty, if an appropriate monetary policy is pursued, it can have no adverse effects whatsoever, except one: It gratuitously increases wealth inequality in society. Abstracting from foreign transactions for simplicity, a fiscal deficit generates an excess of private savings over private investment exactly equal to itself. The government expenditure financed by the fiscal deficit creates additional aggregate demand that increases output and incomes until the additional savings generated out of such incomes exactly match the fiscal deficit (with private investment given).
These additional savings accrue to the savers without their having to reduce their consumption, compared to the initial situation (that is, prior to government expenditure increase). Since savings represent additions to wealth, this amounts to putting extra wealth gratuitously into the hands of the rich (who are primarily the savers). If the same government expenditure was financed by taxation, no matter who was taxed, then there would be no addition to private wealth, and hence no increase in wealth inequality.
Avoiding a fiscal deficit is important for this reason, which is why tax-financed government expenditure should always be preferred to fiscal-deficit-financed government expenditure, even when such taxation does not reduce either private consumption or private investment compared to the initial situation.
Selling public assets, which is analogous to a fiscal deficit, also increases wealth inequality quite gratuitously; and it does so by putting into private hands not just wealth in the form of claims on the government (as a fiscal deficit does), but in the form of public assets, and that too at prices well below the capitalised value of earnings (for otherwise private buyers would not accept them). Instead of taxing away the additional wealth that a fiscal deficit puts into private hands, this strategy actually puts public assets into private hands. This increases wealth inequality for two reasons: First, it does so exactly as a fiscal deficit does; and second, the public asset it puts in private hands is under-priced.
Let us leave aside questions about the strategic role of the public sector that should deter privatisation: As a bulwark against multinational corporations’ propensity to arm-twist a third world country; in making loans available (via public sector banks) to a much wider spectrum of the population than would have occurred otherwise (which had made the Green Revolution possible); and so on. But, even purely as a fiscal strategy, the privatisation of public assets for financing government expenditure, is utterly inexcusable. It betrays either poor economics or a determination to increase wealth inequality.
But what alternative does the government have? The obvious one is wealth taxation. Taxing away the private wealth additionally and gratuitously created by a fiscal deficit leaves private wealth inequality unchanged at its initial level; it does not exacerbate it. Nobody, therefore, should object to it, or even to what comes close to it, namely a larger taxation of profits. Interestingly, when Elizabeth Warren had suggested wealth taxation during her bid for nomination for American Presidency, 18 top billionaires of that country had backed her and suggested higher taxes on themselves.
If the government is unwilling to impose higher wealth or profit taxes, it can raise GST rates on several luxury goods, after consultation with the states. Assuming that working people consume what they earn — and abstracting from foreign transactions — such an increase in indirect taxation matched by an equivalent increase in government expenditure, will still leave post-tax profits in real terms unchanged, while increasing employment and output in the economy. Selling public assets to finance government spending is thus both undesirable and unnecessary.
लोकतंत्र का बदलता व्यवहार
राजेंद्र प्रताप गुप्ता, ( लेखक लोक नीति विशेषज्ञ और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के प्रमुख हैं )
कड़ों वर्षो से एक संस्थान के रूप में लोकतंत्र सरकार का सबसे बढ़िया स्वरूप रहा है। इसका अर्थ है कि चुने हुए लोग ही शासन के अधिकारी हैं। लोकतंत्र एक ऐसा मॉडल है, जहां बहुमत ही तय करता है कि उन पर किसे और कैसे शासन करना चाहिए? अंग्रेजी के ‘डेमोक्रेसी’ शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा से हुआ है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ‘डेमोस’ जिसका अर्थ एक विशेष नगर-राज्य के भीतर रहने वाले समस्त नागरिक और इसका दूसरा हिस्सा है ‘क्रेटोस’ अर्थात सत्ता या शासन। 1863 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने पेंसिलवेनिया में कहा था कि, ‘लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है।’ तबसे यह लोकतंत्र की एक प्रकार से मानक परिभाषा बन गई। यह उस दौर की बात है, जब दुनिया केवल भौतिक रूप से जुड़ी हुई थी। तब नेता या तो अपने कठिन परिश्रम से उभरते-स्थापित होते था या अपने विचारों के कारण। उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होता था। वे विचारक भी होते थे। अब दुनिया डिजिटल दौर से गुजर रही है, जहां लोग कई घंटे वचरुअल संसार में बिताते हैं। यहां लोकतंत्र के मूलभूत तत्वों में ही बदलाव आ रहा है। इंटरनेट डिजिटल संसार में लोगों का पीछा करता है। न केवल पूर्वाग्रह से प्रेरित सूचनाओं की बमबारी करता है, बल्कि लोगों की निजी पसंद और नापसंद पर भी पकड़ रखता है। हमारी ब्राउजिंग और एप्स उपयोग के जरिये हम पर नजर बनाए रखता है। इसी सिलसिले में हम सभी ने कैंब्रिज एनालिटिका जैसा प्रकरण देखा।
इस बीच यह स्पष्ट दिखा कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किस प्रकार इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि झूठे विमर्श के जरिये अमेरिकी संसद तक पर हमला कराकर लोकतांत्रिक संस्थान को अस्थिर करने और चुनी हुई सरकार की राह में बाधा उत्पन्न की गई। चूंकि फर्जी बातों को वास्तविकता का चोला पहनाया जा रहा है तो इससे मतदाताओं को बरगलाना और प्रतिद्वंद्वी की छवि को मलिन करना आसान हो जाएगा। चुनाव मेहनत या छवि पर नहीं, बल्कि विमर्श गढ़कर प्रतिद्वंद्वी को क्षति पहुंचाने पर केंद्रित होंगे। चुनाव में धरातल पर काम का महत्व नहीं रह गया है। अब तो इंटरनेट युग के वर्चुअल संसार में काम का बोलबाला है। नेतृत्व के खास मायने नहीं रहे। चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र सत्ता के दलालों और उन पेशेवर नेताओं के हाथ में सिमटते जा रहे हैं, जो इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जनता को मूर्ख बनाकर और संस्थानों पर काबिज होकर सत्ता में बने हुए हैं। इंटरनेट मीडिया का राजनीति से जितना जुड़ाव होता जाएगा, राजनीति वास्तविकता से उतनी ही कटती जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार में व्यापक बदलाव आया है। ऐसे में कोई हैरानी नहीं कि वैश्विक नेताओं के इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर गाज गिर रही है, लेकिन इससे खास मदद नहीं मिलने वाली।
इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल ताकतवर तिकड़मियों के पक्ष में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने लिए जारी रहेगा। ऐसे में लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थानों पर दृष्टि डालने के लिए नए तौर-तरीके खोजकर कदम उठाना आवश्यक हो गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि नागरिकों एवं शासन के नजरिये से इंटरनेट मीडिया लोकतंत्र के जांचे-परखे रूप को विरुपित कर रहा है। प्रख्यात फ्रांसीसी विचारक मांटेस्क्यू ने सत्रहवीं शताब्दी में कहा था कि ‘व्यापक जनकल्याण के अभाव में विभिन्न गुटों के बीच संघर्ष से लोकतंत्र के नष्ट होने की आशंका होती है, जहां प्रत्येक गुट व्यापक सार्वजनिक कल्याण की कीमत पर अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति के प्रयास में होता है।’ आज की तारीख में इंटरनेट मीडिया को उन गुटों की संज्ञा दी जा सकती है। जब हम वर्चुअल संसार की हलचल को देखते हैं तो यही प्रतीत होता है कि इंटरनेट मीडिया लोकतंत्र के साथ असंगत है। यह लोकतंत्र के निर्णय और विकल्पों की वैधानिकता के समक्ष जोखिम बढ़ाता है। इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल एवं प्रसार ने लोकतंत्र के आधारभूत तत्वों का अवमूल्यन किया है। यह लोगों की धारणाएं प्रभावित कर किसी विशेष विचारधारा, विमर्श या शख्सीयत के पक्ष में मतदान करने का संभावित हथियार बन सकता है।
पहले लोग चुनाव में जीतने के लिए काम को तवज्जो देते थे। वे चुनाव के लिए प्रचार का भी सहारा लेते थे, लेकिन अब यह सब वचरुअल दुनिया से तय हो रहा है। अक्सर उसमें धारणा, छल-प्रपंच और जोड़तोड़ का सहारा लिया जाता है। वास्तव में चुनाव कल्पित धारणा और झूठे विमर्श पर जनमत संग्रह बन गए हैं। समय के साथ लोकतंत्र एवं इंटरनेट मीडिया के बीच की यह दुरभिसंधि और गहरी होकर खतरनाक होती जाएगी। कुछ दशकों पहले तक सामाजिक कार्यकर्ता और जमीनी स्तर पर सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर चुनाव जीते जाते थे, लेकिन अब इंटरनेट मीडिया की तिकड़मों के सहारे जीत तय होने लगी है। ये बिचौलिये और सत्ता के दलाल हैं, जिन्होंने नेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिसने सत्ता कायम रखने के लिए लोकतंत्र को अपनी बपौती बना लिया है। राजनीति अब सेवा करने वाले नेतृत्व से नहीं, बल्कि सेलेब्रिटी वाले पहलू से पहचानी जाने लगी है। इस सबका जिम्मेदार है इंटरनेट मीडिया।
मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया और अब उसकी जगह इंटरनेट मीडिया ले रहा है। जनता पर इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए मैं उसे मनोवैज्ञानिक मीडिया कहूंगा। कुछ साल पहले एक लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान मैंने कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब इंटरनेट मीडिया दिग्गज ही न्यूज चैनल बन जाएंगे और वक्त के साथ चीजें काफी स्पष्ट भी होती जा रही हैं। इंटरनेट मीडिया में न केवल समाचार दिखाने, बल्कि समाचार ‘गढ़ने’ की अपार क्षमता है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यह प्रसार का नहीं, बल्कि प्रभावित करने का मसला अधिक है। हाल में दुनिया के एक दिग्गज अरबपति को मात्र एक ट्वीट के कारण 15 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। यदि हम ऐसी बातों के देश पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो इससे युद्ध तक भड़क सकता है। भविष्य में राष्ट्रों पर इसका और व्यापक प्रभाव होगा। ऐसे में हमें इंटरनेट मीडिया के दौर में लोकतंत्र से जुड़े विमर्श का सांचा बदलना होगा। हमें नए दौर के लोकतंत्र की आवश्यकता है और अब इस पर बहस अवश्य शुरू होनी चाहिए।
विधानसभा हो ही क्यों ?
उमेश चतुर्वेदी
दिल्ली की राज्य सरकार और उसके मुखिया उपराज्यपाल के अधिकारों पर बहस तेज है। इसकी वजह है‚ संसद में पेश ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अधिनियम‚ 2021 इसमें उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाने की बात है। लगातार दो चुनावों में भारी बहुमत से जीत कर सरकार बना चुके अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी (आप) ने इस विधेयक के बहाने जो बहस शुरू की है‚ उसमें कहा है कि भारी बहुमत से जीती सरकार के पास अन्य राज्य सरकारों की तरह अधिकार क्यों न होंॽ ॥ 1858 में देश पर महारानी विक्टोरिया का शासन होने के बाद दिल्ली को पंजाब राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। महाभारत काल से लेकर सल्तन काल होते हुए मुगल वंश के दौरान तक देश की राजधानी रही दिल्ली का अंग्रेजों ने स्वतंत्र प्रशासनिक अस्तित्व रखने की बजाय पंजाब राज्य के मेहरौली जिले का अंग बना दिया था। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का फैसला किया तो 12 दिसम्बर‚ 1911 को दिल्ली को पंजाब से अलग करके सीधे केंद्रीय शासन के अधीन ले लिया और उसे चीफ कमिश्नर के हवाले कर दिया। आजादी मिली तो भारत में तीन ऐसे इलाके थे‚ जिनका शासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन चीफ कमिश्नर की देखरेख में चलता था। आजादी के बाद संविधान सभा की बहसों में सवाल उठा कि दिल्ली‚ अजमेर और कुर्ग जैसे चीफ कमिश्नर शासित राज्यों की भावी शासन व्यवस्था क्या होगी। संविधान सभा ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पट्टाभि सीतारमैया की अध्यक्षता में समिति बना दी। सीतारमैया ने उस वक्त लोकतांत्रिक दुनिया की चार राजधानियों वाशिंगटन डीसी‚ लंदन‚ ओटावा और कैनबरा की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट में दिल्ली में विधानसभा की सिफारिश कर दी। बेशक‚ केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति के अधिकार को सर्वोच्च माना।
ध्यान रखने की बात है कि तब दिल्ली की जनसंख्या करीब छह लाख थी और करीब 82 प्रतिशत आबादी शहरी। सवाल लाजिमी है कि आखिर‚ जिस इलाके का स्थानीय शासन नगर निगम या नगर पालिका के जरिए चलाया जा सकता था‚ उसके लिए विधानसभा की अनुशंसा ही क्यों की गई। संविधान विशेषज्ञ और लोक सभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप कहते हैं कि दिल्ली में विधानसभा की जरूरत ही नहीं थी। कुछ स्थानीय नेताओं की लाल बत्ती की महवाकांक्षा के लिए इसे राज्य बना दिया गया। दिल्ली में चूंकि एक बार विधानसभा बन चुकी थी‚ इसलिए उसके खत्म किए जाने को एक वर्ग स्वीकार नहीं कर पाया और आए दिन इसकी मांग उठती रही। 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार ने भी ऐसा वादा किया था। लेकिन वह सरकार जब तक कोई कदम उठाती‚ खुद ही अपने अंतवरोधों के चलते ध्वस्त हो गई। इस बीच भारतीय जनता पार्टी‚ जनता दल और कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व विधानसभा की बहाली की मांग करता रहा। इसे देखते हुए राजीव सरकार ने 1987 में न्यायमूत सरकारिया की अध्यक्षता में समिति बनाई। बाद में उन्हें प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाए जाने पर न्यायमूत बालाकृष्णन को जिम्मेदारी दी गई जिन्होंने 1989 में अपनी रिपोर्ट में सीतारमैया समिति की बात को ही बढ़ाया। दिल्ली में स्थानीय व्यवस्थाओं को छोड़कर केंद्र की सर्वोच्चता पर बल दिया।
भारी बहुमत से सत्ता में आई केजरीवाल सरकार का महवाकांक्षी होना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल है कि भारी बहुमत से नगर या ग्राम पंचायत में जीत मिलती है तो क्या उसे केंद्रीय सत्ता जैसे अधिकार मिल जाएंगे। बहुमत किसी सरकार के अधिकारों के बढ़ाने और संविधान की नई व्याख्या का जनमत संग्रह नहीं होता। दिल्ली बनाम केंद्र की लड़ाई के बीच से इस आधार पर किसी का ध्यान नहीं है। हालांकि जब इस आधार पर चर्चा होगी तो संभवतः सवाल उठने लगे कि नगर निगम से शासित किए जा सकने वाले दूसरे नगरों की तरह आखिर दिल्ली में ही राज्य सरकार क्यों होनी चाहिए। मुंबई‚ कोलकाता‚ हैदराबाद‚ चेन्नई और बेंगलुरू का स्थानीय शासन नगर निगमों के जरिए चलाया जा सकता है‚ तो फिर दिल्ली में ही विधानसभा क्यों ॽ
महिलाओं को उपहार नहीं, सदन में जगह चाहिए
नमिता भंडारे
महिलाओं के लिए यात्रा रियायतों, गृहिणियों के लिए वेतन, एलपीजी सिलेंडर, सरकारी नौकरी में आरक्षण और यहां तक कि मुफ्त वाशिंग मशीन का भी वादा किया जा रहा है। चुनावी संकेतों को समझने के लिए बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। चुनाव कोई भी हो, महिला वोटरों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनाव और राजनीति में महिलाओं के बड़े महत्व के बावजूद एक तथ्य बहुत कटु बना हुआ है कि किसी भी चुनाव में महिला प्रतिद्वंद्वियों की संख्या कम रहती है।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी के 291 घोषित उम्मीदवारों में से महज 50 महिलाएं हैं। मतलब वहां पार्टी के कुल उम्मीदवारों में महज 17 प्रतिशत महिलाएं हैं। हालांकि, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 41 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा था। फिर भी, पश्चिम बंगाल इस मामले में केरल से आगे है। केरल में महिला उम्मीदवारों की संख्या नौ प्रतिशत ही है। केरल महिला कांग्रेस की प्रमुख लथिका सुबाश ने इसके लिए अपना विरोध भी जताया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) में 85 में से 12 महिला उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 115 उम्मीदवारों में 15 महिलाएं। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक द्वारा शुरुआती दौर में घोषित 171 उम्मीदवारों में से केवल 14 और द्रमुक के 173 उम्मीदवारों में से 12 महिलाएं हैं। असम में भी शुरुआती 223 घोषित उम्मीदवारों में से महज 19 महिलाएं थीं। चुनाव लड़ने वाली महिलाओं के ऐसे आंकड़े हर हाल में दयनीय हैं। महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से एक संगठन की सह-संस्थापक तारा कृष्णस्वामी ने इसे लोकतंत्र की भयावहता करार दिया है। महिला प्रतिनिधियों की संख्या चिंता पैदा करती है। केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य लिंग आधारित विकास संकेतकों के मामले में अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन जब विधानसभा या लोकसभा के लिए महिला उम्मीदवारी की बात आती है, तो वे भी पिछड़ जाते हैं। विधानसभाओं और संसद में सीटों पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की घोषणापत्रों में बात करना केवल कथनी है। किसी पार्टी को इस दिशा में पहल करने की शुरुआती जरूरत भी महसूस नहीं हुई है। सियासी पार्टियां महिलाओं को आगे लाने की बस बात करती रहती हैं। यह बात भी अब बहुत पिट चुकी है। जब हम आधी आबादी हैं, तब विधायिका में किसी चीज के लिए हम समझौता क्यों करें? मसला प्रतिनिधित्व का है। अब पुरुष ऐसी नीतियों पर निर्णय लेना जारी नहीं रख सकते, जो महिलाओं को प्रभावित करती हैं, चाहे वह संशोधित गर्भपात विधेयक हो या किशोर न्याय कानून में बदलाव। प्रतिनिधित्व से भी अधिक जरूरी है कि महिलाएं मौके की जगहों-पदों पर काबिज हों, यह महिलाओं का अधिकार भी है। जब हम सार्वजनिक स्थानों के बारे में सोचते हैं, तो हम अपनी कल्पनाओं को उद्यान, सड़क और सार्वजनिक परिवहन तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों में संसद और विधानसभाएं भी तो शामिल हैं। इसमें उच्च न्यायपालिका, श्रम बल, उच्च शिक्षा, कार्यालय और खेल भी शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र व स्थान से महिलाएं कमोबेश गायब हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की हालिया सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक महिला जज व उच्च न्यायालयों में छह प्रतिशत से भी कम महिला जज सेवारत हैं। सार्वजनिक रिक्त पदों पर किसे रखा जाए का सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाता है, जब महामारी के समय महिलाओं को घर के अंदर धकेला जा रहा हो। यह वाकई चिंता की बात है, अगर श्रम बल में महिलाओं की भागीदार घट रही है। नि:शुल्क वाशिंग मशीनों के खिलाफ भला कौन जा सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए इसका वितरण पुरुष प्रधान राजनीतिक दलों के इस विश्वास या सोच को दर्शाता है कि महिलाओं की वास्तविक जगह वह कहां समझते हैं। कोई इन राजनीतिक दलों को बताए कि महिलाओं की जगह वॉशिंग मशीन के पास ही नहीं है, संसद व तमाम विधाई सदनों में है। और यह समय है, जब महिला मतदाता अपना यह संदेश सुना दें।
