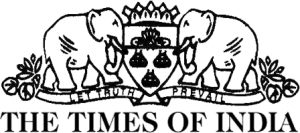23-11-2016 (Important News Clippings)
To Download Click Here
Now reform political funding
If we have the will, here’s how to make a lasting impact on black money
The two weeks old demonetisation tsunami is still reverberating through the nation’s socioeconomic fabric. It will be months before its impact can be fully understood, but the economic and political landscape has already been rearranged.Political bickering over long bank and ATM queues dominated media reports for the first two weeks. Now there is increasing coverage on the expected benefits – or lack thereof, depending on which side you are on – as well as various short and long term effects on the economy. This column will focus on how to cleanse politics of illicit, tax-evaded, ‘black money’.
It is bizarre that some otherwise reasonable people have said demonetisation will not impact black money. Sure, the currency portion of illicit assets is relatively small, with much more held in gold, real estate etc. But being by far the most fungible, cash is the most crucial part of the black economy. And it is by no means insignificant, with an estimated Rs 3 lakh crore and perhaps more now expected to be extinguished.This one-time flushing of a chunk of black money is a significant blow to its users, but a lasting impact requires several other steps. It would be good for the government to tackle head-on such whispered allegations that agents are arranging to rehabilitate some of this cash, supposedly through Jan Dhan accounts and suchlike. Quick disproval, or punitive action if true, would add to the credibility of demonetisation.
The good news is that unlike 1978, when the last demonetisation saw black money get hit but come roaring back, the ground realities are very different now. Mandatory linkage to PAN and Aadhaar cards for most transactions will be one of the fundamental ways to check the re-generation of black money. But the single biggest step would be to start cleaning up political funding.Some years ago the Law Commission of India had sought public suggestions on electoral reforms, whereupon i had given written recommendations to it and to the Election Commission. Though the Law Commission’s subsequent 2015 report contained many laudable ideas for electoral transparency, its chapter on ‘election finance reform’ stopped short of anything truly radical or transformative.
The most important aspect of election finance reform is to shift the focus from limiting campaign expenses to rigidly enforcing the legitimacy and traceability of the money trail. Our decades’ long, utopian thrust on capping campaign expenses has not worked, it has only pushed money under the carpet. This is the root cause, the motivation for black money, and for the mechanisms that generate it.The fear that allowing higher campaign expenses would somehow undermine democracy is unfounded, and there are better ways of ensuring a level playing field than expense caps. In any event, for all practical purposes the caps are meaningless, and have only incentivised the use of unsavoury funds from dubious sources.
The reality is that money is a necessary but far from sufficient ingredient for electoral success. Ironically, even billionaire Donald Trump’s successful campaign relied on a budget that was half of his opponent’s!Rather than expense caps, it is far, far more important to ensure that campaign funds are from traceable, tax-compliant sources. Thus, the floor of Rs 20,000, below which political contributions can be received anonymously, must be drastically lowered. This is the single greatest window of abuse, with huge sums of black money being transacted without any traceability.
Though i had earlier favoured a floor of Rs 5,000, i now believe it needs to be Rs 1,000 or even Rs 500. That would allow genuine on-the-spot donations, say at political rallies, but make it far harder to channel large amounts of illicit funds via countless ‘nameless donors’.Next, there must be state funding to help level the playing field between the wealthy and the popular. Like elsewhere, our state funding should be given as matching funds to candidates and parties, equivalent to the amount of traceable, tax-compliant funds that they raise.
In fact, small donations must be further incentivised over big ones, say with five-times matching funds for every individual Rs 1,000 of tax-compliant funds raised. Together, all this will be a boon to non-wealthy but popular candidates and parties.Finally, audits of candidates’ and parties’ accounts must be made mandatory, and the tax exemptions they now receive be limited to funds that are traceable and tax-compliant. Most importantly, the EC’s powers must be enhanced to enforce such audits, along with punitive powers ranging from mild penalties all the way to disqualifications. It is amazing that the EC, arguably India’s most credible institution, does not have these powers.
The past three months have been momentous, with passage of the previously intractable GST bill, then surgical strikes across the LoC, and now demonetisation. Like its policies or not, it is undeniable that after a period of drift, the Modi government seems to be on a roll.This new, no-longer-business-as-usual scenario is aptly described by an aphorism from The Wizard of Oz, “We’re not in Kansas anymore.” So, how out of the box is the PM prepared to be? As it happens, he reportedly mooted the idea of state funding of elections at last week’s all-party meeting. Irrespective of our political leanings, that deserves support and championing by thinking citizens.
Date: 23-11-16
Get down not dirty
Crawling may be the biggest fitness trend of 2017 and India is ready for it
Being human is about walking upright, anthropologists say. It took millions of years of evolution for primates to go bipedal. Modern humans are celebrated if they can cover long distances on two legs. Runners are the most coveted of singletons. But in a queer counter-trend, these days many gym instructors are telling their clients to drop down on all fours instead. Apparently the isometry of crawling is terrific for building strength holistically from wrists and shoulders through to hips, ankles and toes. There’s also the theory that when you crawl you press reset on your central nervous system and revisit your baby being and that really helps improve core stability – both physical and psychological.
Right now this concept can’t be tested on a mass scale on Indians because if we went down on all fours then the queues outside banks would get even longer – and that wouldn’t reset the nervous system in any pleasant way whatsoever. But in the goodness of time it may prove a great fit for the heart, cholesterol, cellulite and love handles of our country. It will bloom where desh ki dharti is already heavily fertilised with chamchagiri. There will be no stopping the kowtowing courtiers, cronies, bhakts and maska-maalishers once they trust that crawling won’t even cost them their knees.
But not everybody is buying the PR pitch for crawling. For example it’s supposed to be a topping exercise because it keeps you working hard to hold a position under repeated tension. For a lot of people that’s an exact description of their day job – the one that has them running to the gym afterwards. And what they really want to do is fly.
अचल संपत्ति में काले धन पर रोक से किस पर पड़ेगी चोट?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को काले धन पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ की घोषणा के बाद से अब तक अचल संपत्ति क्षेत्र की कंपनियों के शेयर करीब 25 प्रतिशत गिर चुके हैं। निवेशकों को आशंका है कि आवासीय अचल संपत्ति की मांग में तेज गिरावट आएगी क्योंकि इसमें भारी मात्रा में काला धन लगा हुआ है। इस भय में काफी सच्चाई है। मोदी की घोषणा के बाद बाजार में गिरावट आई। बिल्डरों का मानना है कि अगली एक-दो तिमाही में कीमतें 25 प्रतिशत तक घट सकती हैं।मोदी ने कहा है कि आने वाले दिनों में सरकार बेनामी संपत्तियों पर हमलावर रुख अपनाएगी। मोदी को इस वादे पर तेजी से अमल करना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र में लगे काले धन को हरसंभव तरीके से रोकना चाहिए। ऐसी चर्चा चल रही है कि वह इस क्षेत्र में नकद लेनदेन की सीमा तय कर सकते हैं। यानी एक खास सीमा से अधिक राशि का भुगतान चेक के माध्यम से ही करना होगा।अचल संपत्ति के प्राथमिक बाजार के अलावा द्वितीयक बाजार में भी नकदी का बोलबाला है। विक्रेता अक्सर अपनी संपत्ति की कीमत कम करके बताते हैं ताकि कर बचाया जा सके। यह काला धन पैदा होने की वजह बनता है।लंबी अवधि के दौरान मोदी के इस अभियान से कुछ सकारात्मक चीजें निकलेंगी। देश में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये कीमतें दुनिया में सबसे ऊंची मानी जा सकती हैं। इसके अलावा किसी भवन निर्माता को जमीन खरीदने के बाद अनिवार्य सरकारी मंजूरी मिलने में दो साल का अरसा लग ही जाता है। इस अवधि के दौरान जमीन खाली पड़ी रहती है जिससे उसकी लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है। इतना ही नहीं भवन निर्माताओं को अक्सर कर्ज भी सामान्य लोगों की तुलना में काफी ऊंची दर पर मिलता है। यही वजह है कि वे अक्सर महंगी परियोजनाएं ही शुरू करते हैं। आजकल कोई सस्ते आवास की बात नहीं करता।अचल संपत्ति में काले धन पर प्रहार होने के साथ ही मांग में जबरदस्त कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जमीन की कीमतें भी कम हो सकती हैं। इससे भवन निर्माताओं के पास सस्ते मकान बनाने की गुंंजाइश पैदा होगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सभी मंजूरियों को पारदर्शी बनाया जाए और नौकरशाहों के पास कोई विशेषाधिकार नहीं रहने दिया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भवन निर्माताओं की जमीन लंबे समय तक खाली नहीं पड़ी रहेगी।यहां पर राज्यों को आगे आना होगा। हर राज्य के अपने नियम कायदे होते हैं जिनसे वह अचल संपत्ति कारोबार को संचालित करता है। यही वजह है कि देश में ऐसे भवन निर्माताओं का अभाव है जो पूरे देश में कारोबार करते हों। प्रत्येक कारोबारी एक या दो राज्यों में ही कारोबार करता है क्योंकि सभी राज्यों के कारोबारियों से तालमेल बिठा पाना आसान काम नहीं है। कुछ लोग राष्टï्रीय स्तर पर काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन जल्दी ही अपने कदम वापस खींच लेते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हर शहर का अपना अलग बाजार है।घर खरीदने वालों को संरक्षण प्रदान करने वाले नियम अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि राजनेता और नौकरशाह भवन निर्माण कारोबारियों से धन उगाहने की कोशिश न करें। बहरहाल, पुरानी व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले लोग ऐसे किसी भी कदम का जमकर विरोध कर रहे हैं जिसे समझा जा सकता है। इसके अलावा भवन निर्माता जो रिश्वत देते हैं वह हमेशा नकद में होती है। इसकी मात्रा भी बहुत अधिक होती है। भवन निर्माताओं को निरंतर इस नकदी को निरंतर बरकरार रखना होता है। यह सारा काला धन होता है। यह भी एक बड़ी वजह है जिसके चलते भवन कारोबारी नकदी का प्रयोग करते हैं। जब तक इस समस्या को हल नहीं किया जाता है। तब तक अचल संपत्ति क्षेत्र से काले धन को खत्म करने का कोई भी प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो सकता है।मोटे तौर पर ऐसा इसलिए क्योंकि कारोबार में नकदी की यह उपस्थिति बड़े कारोबारियों को इससे दूर रखती है। सन 1990 के दशक में कई कारोबारियों का कहना था कि वे अपनी खाली पड़ी जमीन में अचल संपत्ति की बड़ी परियोजनाएं शुरू करेंगे लेकिन एक बार जब उनको पता चला कि यहां इतने बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन होता है तो उन्होंने अपने हाथ वापस खींच लिए।यह सडऩ कितनी गहरी हो चुकी है यह जानने के लिए मैं पाठकों से अनुरोध करूंगा कि वे कोबरापोस्ट द्वारा अक्टूबर 2014 में की गई एक खोजी रिपोर्ट को पढ़ें। 18 महीनों तक चली ब्लैक निंजा कूट नाम वाली इस खोजी रिपोर्ट में वेबसाइट ने पाया कि 35 कंपनियां काले धन में लेनदेन करने के लिए तैयार थीं। ये कंपनियां किसी संपत्ति के मूल्य का 10 से लेकर 90 फीसदी तक नकद लेने को तैयार थीं। कुछ कारोबारी अपनी परिसंपत्तियां बिना नियामकीय मंजूरी के ही बेच देने को तैयार थे। जबकि ऐसा करना अवैध था। कुछ अन्य कारोबारियों ने विदेशों में हवाला के जरिये पैसा ले लिया। बहरहाल एक कहावत है कि अच्छी शुरुआत का मतलब है मानो आधा काम हो गया।
Date: 23-11-16
गांव हुए मायूस
ग्रामीण भारत के दु:स्वप्न का अंत होता नजर नहीं आ रहा है। लगातार दो वर्षों के सूखे के बाद इस साल बेहतर मॉनसून की मेहरबानी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आखिरकार सुधार होता दिख रहा था। आशा जताई गई कि खरीफ उत्पादन में भारी बढ़ोतरी से ग्रामीण उपभोग में इजाफा समग्र आर्थिक वृद्घि को तेजी देता। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का जो फैसला किया, वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बुरी तरह शिकंजे में कस रहा है।असल समस्या है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत हद तक नकद लेनदेन पर आधारित है, जबकि शहरी मध्यम वर्गीय लोगों के पास ऑनलाइन, मोबाइल मनी के अलावा क्रेडिट और डेबिट कार्ड जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं। यह स्वाभाविक कमजोरी परिदृश्य को और बदतर बना देती है कि 90 फीसदी से अधिक ग्रामीण इलाके बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं, जिसके कारण नए नोटों को उन तक पहुंचाने की सरकारी कोशिशें रंग नहीं ला रही हैं। सिर्फ एक आंकड़े से यह दर्दनाक तस्वीर स्पष्टï हो जाती है कि जबसे सरकार ने नोटबंदी का निर्णय किया, उसके 10 दिनों के भीतर सरकार अखिल भारतीय स्तर पर केवल 10 फीसदी नकद निकासी को ही संभव बना पाई है।हैरानी की बात नहीं कि इसके कारण नकदी की किल्लत हो गई, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खस्ताहाल कर दिया है। विश्लेषकों के अनुसार ग्रामीण मजदूरी दरें नवंबर, 2013 से ही गिरावट की शिकार हैं और यह गौर करने वाला पहलू है कि इस दौरान सूखे की मार बहुत प्रभावी रही। कुल मिलाकर ग्रामीण आमदनी सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। विमुद्रीकरण के समय को लेकर भी इसके तार जोड़े जा रहे हैं क्योंकि यह घोषणा कृषि से जुड़ी गतिविधियों के बेहद व्यस्त दौर के बीच में हुई है, जहां किसान या तो खरीफ फसल की कटाई कर रहे थे या फिर रबी फसल की बुआई में लगे थे। तमाम किसानों को अपने उत्पादों के लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं क्योंकि खरीदारों के पास नकदी नहीं है, जिसके कारण कीमतों में भारी गिरावट आई है। साथ ही पहले कटाई करके फसल बेचने वाले खुशकिस्मत किसानों को एक और बदनसीबी ने आ घेरा है क्योंकि फसल बेचने के बदले उन्हें जो नोट मिले, वे अब किसी काम के नहीं रहे। ऐसे में इन किसानों के पास नई फसल की बुआई के लिए बीज और खाद जैसी बुनियादी चीजों को खरीदने के लिए नकदी नहीं हैं।ग्रामीण इलाकों से तमाम दर्दनाक वाकयों के बाद सरकार की भी आंखें खुलीं और उसने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए। जैसे किसानों के लिए नकद निकासी की सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी। इसके अलावा फसल बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए 15 दिनों की मोहलत भी बढ़ा दी। कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव पर शुरुआत में विरोध जताने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह मांग भी मान ली कि किसानों को 500 रुपये के पुराने नोट के बदले बीज खरीदने की इजाजत दी जाए। मगर बीज खरीदारी में रियायत जैसे कदम उठाने में बहुत देर कर दी। जैसे साल दर साल केवल 30 फीसदी बीज ही बदले जा रहे हैं। दुखद पहलू है कि रबी फसल में गेहूं बुआई के लिए 15 से 20 नवंबर का समय आदर्श माना जाता है। अगर देर से बुआई होती है और खासतौर मार्च में अगर तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है तो इससे फसल उत्पादन प्रभावित होगा। साथ ही यह राहत उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे अहम उत्पादों के लिए नहीं दी गई है, जिनकी कमी से उत्पादन घटकर आधा भी रह सकता है। वर्ष 2014-15 के दौरान कृषि क्षेत्र में 0.2 फीसदी की गिरावट आई, जबकि 2015-16 के दौरान इसमें महज 1.2 फीसदी का इजाफा हुआ। अगर कमजोर आधार की भी बात करें तो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में 1 फीसदी से भी कम बढ़ोतरी का अनुमान है। स्पष्टï है कि ग्रामीण आपदा को दूर करने के लिए अभी काफी कुछ करने की जरूरत है।
जीएसटी में राज्यों की भूमिका
आधे से अधिक राज्यों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर संबंधी संविधान संशोधन पर मोहर लगाने के बाद इस व्यवस्था का लागू होना सुनिश्चित हो गया है। जीएसटी के प्रस्ताव में अब कई कमियां दूर हो गई हैं। पूर्व में सभी वस्तुओं पर एक ही दर से टैक्स प्रस्तावित था, जैसे साइकिल तथा लक्जरी कार पर। प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान प्रस्ताव में चार दरें हैं-5, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत। आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं पर पांच प्रतिशत से न्यून कर वसूल किया जाएगा, जबकि तंबाकू तथा लक्जरी कार पर 28 प्रतिशत की दर से। यह कदम सही दिशा में है, किंतु अभी इसमें एक पेच बाकी है। किस माल को किस दर में रखा जाएगा, यह तय होना बाकी है। मसलन माचिस तथा साइकिल पर पांच प्रतिशत से टैक्स वसूला जाएगा या 18 प्रतिशत से, यह अभी तय नहीं है। जीएसटी को सकारात्मक बनाने के लिए आम आदमी द्वारा खपत किए जाने वाले अधिकाधिक माल को पांच प्रतिशत के स्लैब में रखा जाना चाहिए।
28 प्रतिशत की दर के स्लैब के दायरे को भी बढ़ाने की जरूरत है। वर्तमान में इसमें तंबाकू, साफ्ट ड्रिंक तथा लग्जरी कार सम्मिलित किए गए हैं। इसका दायरा फास्ट फूड, एयर कंडीशनर, ब्रैंडेड कपड़े, चाकलेट आदि हानिप्रद अथवा गैर जरूरी वस्तुओं पर बढ़ा दिया जाना चाहिए। यह भी प्रस्तावित है कि अगले पांच वर्षों तक इन माल पर 12 प्रतिशत का सेस वसूल किया जाएगा, जिससे इन पर कुल 40 प्रतिशत का टैक्स देय होेगा। इस सेस को 5 वर्षों तक सीमित करने का औचित्य नहीं है। यदि यह माल आज जनता के लिए हानिप्रद है तो पांच वर्ष बाद भी हानिप्रद ही रहेंगे। अत: 28 प्रतिशत के स्लैब को स्थाई रूप से बढ़ाकर 40 प्रतिशत या इससे भी अधिक कर दिया जाना चाहिए। जीएसटी की एक और कमी दूर हो गई है। पूर्व में प्रस्तावित था कि सभी छोटे और बड़े उद्योग पर समान दर से टैक्स आरोपित किए जाएंगे। ऐसा होते ही छोटे उद्योगों का स्वाहा निश्चित था। वर्तमान प्रस्ताव में छोटे व्यापारियों एवं उद्योगों को
वर्तमान में मिलने वाली छूट में बढ़त की गई है। यह कदम भी सही दिशा में है।जीएसटी की मुख्य समस्या रह जाती है राज्यों की स्वायत्तता की। वर्तमान में विभिन्न माल पर अपनी जरूरत के अनुसार टैक्स वसूल करने को राज्य स्वतंत्र है। मसलन एक राज्य साइकिल पर 10 प्रतिशत से और दूसरा राज्य इस पर 15 प्रतिशत से टैक्स वसूल कर सकता है। जीएसटी लागू होने के बाद किस माल पर किस दर से टैक्स वसूला जाएगा, यह जीएसटी काउंसिल द्वारा तय किया जाएगा। इसके बाद पूरे देश में सभी राज्यों द्वारा उसी दर से टैक्स वसूल किया जाएगा। पेट्रोलियम को छोड़ अन्य सभी माल पर टैक्स की दर तय करने का राज्य का अधिकार छिन जाएगा। मूल रूप से टैक्स दर का यह एकीकरण नकारात्मक है। संविधान के मूल ढांचे के भी यह विरुद्ध है, परंतु आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं पर न्यून दर से टैक्स वसूलने तथा छोटे उद्योगों को छूट देने के कारण जीएसटी के इस नकारात्मक पहलू को बर्दाश्त करना होगा। तीन मुद्दे शेष रह जाते हैं। पहला है जीएसटी व्यवस्था पर नियंत्रण का। केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि पूरी प्रक्रिया पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो। सेंट्रल एक्साइज विभाग द्वारा ही जीएसटी लागू किया जाए। इसके विपरीत कुछ राज्यों की मांग है कि छोटे करदाताओं यानी 1.5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से कम व्यापार करने वालों पर नियंत्रण राज्य सरकार का हो। इन छोटे करदाताओं पर केंद्र सरकार द्वारा निगरानी मात्र रखी जाए। राज्यों के कामर्शियल टैक्स अधिकारियों की च्वाइंट एक्शन कमेटी ने छोटे व्यापारियों पर राज्य का नियंत्रण न स्वीकार किए जाने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है। इन अधिकारियों की मांग घूस की कमाई को बचाने की है। करदाता को कोई अंतर नहीं पड़ता है कि टैक्स की वसूली भ्रष्ट राज्य तंत्र द्वारा की जाएगी अथवा भ्रष्ट केंद्रीय तंत्र द्वारा। सिटिजन फोरम फॉर सिविल लिबर्टी के गोपाल कृष्ण कहते हैं कि राज्य के आइएएस एवं आइपीएस अधिकारी ही केंद्र की व्यवस्था का डेपूटेशन पर संचालन करते हैं। यदि ये राज्य में भ्रष्ट थे तो केंद्र में ईमानदार कैसे हो जाएंगे?
आम आदमी के लिए दोनों एक समान हैं। बड़े करदाताओं के लिए केंद्र की व्यवस्था पर सभी सहमत हैं। इसलिए छोटे करदाताओं पर भी केंद्र का नियंत्रण करना चाहिए, जिससे करदाताओं को दो तंत्रों को अलग अलग घूस नहीं देनी पड़ेगी।दूसरा मुद्दा है वोट के वजन का। वर्तमान में जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों को एक-एक वोट दिया गया है। छोटे और बड़े राज्यों में भेद नहीं किया गया है। यह ऐसे हुआ कि महाराष्ट्र और मणिपुर को लोकसभा में बराबर सांसद आवंटित कर दिए जाएं। तमिलनाडु ने यह मुद्दा उठाया है, जो कि सही है। काउंसिल में राज्यों के वोट को राज्यों के अनुपात में वजन देना चाहिए। तीसरा मुद्दा है केंद्र के वीटो पॉवर का। वर्तमान व्यवस्था में जीएसटी काउंसिल में 33 प्रतिशत वोट केंद्र को दिए गए हैं। सभी राज्यों को मिलाकर 67 प्रतिशत वोट दिए गए हैं। साथ-साथ व्यवस्था है कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 75 प्रतिशत वोट मिलना जरूरी है। ऐसे में केंद्र को अनकहा वीटो पॉवर हासिल हो जाता है। मान लीजिए कि सभी राज्य चाहते हैं कि साइकिल पर पांच प्रतिशत से टैक्स वसूल किया जाए, लेकिन केंद्र चाहता है कि इस पर 18 प्रतिशत से टैक्स वसूल किया जाए। सभी राज्यों के सम्मिलित 67 प्रतिशत वोट न्यून दर के पक्ष में पड़े, परंतु प्रस्ताव के पारित होने के लिए चाहिए जरूरी 75 प्रतिशत वोट से यह कम है इसलिए यह प्रस्ताव गिर जाएगा। बिना केंद्र की सहमति के काउंसिल में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है।
राज्य वास्तव में पदच्युत कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था नाजायज है। वास्तव में केंद्र को वोट देने का अधिकार देने की जरूरत ही नहीं है। केंद्र का काम है कि राज्यों द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार व्यवस्था चलाए।जीएसटी व्यवस्था सही दिशा में चल रही है। कार्यान्वयन के स्तर पर आम आदमी के उपयोग के सभी माल को पांच प्रतिशत के स्लैब में रखा जाना चाहिए तथा सभी हानिप्रद एवं गैर जरूरी माल को 40 प्रतिशत के स्लैब में। 28 प्रतिशत के स्लैब को स्थायी रूप से 40 प्रतिशत बना देना चाहिये। जीएसटी के ढांचे में तीन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। केंद्र का एकल नियंत्रण बनना चाहिए। दो के स्थान पर एक जगह घूस वसूल की जाए तो उत्तम है। दूसरे, जीएसटी काउंसिल में राज्यों के वोट का वजन जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। अन्यथा केंद्र द्वारा मुट्ठी भर छोटे राज्यों को साथ लेकर देश की बड़ी जनता के विरुद्ध कदम उठाया जा सकता है। तीसरे, जीएसटी काउंसिल में केंद्र को शून्य वोट देना चाहिए। इससे केंद्र का अनकहा वीटो समाप्त हो जाएगा और बचा खुचा संघीय ढांचा बचा रहेगा।
[ लेखक डॉ. भरत झुनझुनवाला, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और आइआइएम बेंगलुरु में प्रोफेसर रह चुके हैं ]
The buck stops with the States
Given the diversity in development between States, it is only prudent that land acquisition laws be customised to suit local requirements

The need for State-specificity
The Constitution allows for a State law to override the Central law in case of the Concurrent List if the former gets presidential assent. This exception was made to provide for a ‘genuine hurdle’ in implementing (or genuine necessity to deviate from) the Central law due to challenges peculiar to a region. What this genuine hurdle is, is a point that can be debated.
The second issue seems to be with respect to the particular Central law, that is, the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (LARR) Act, 2013. The charge is that the Social Impact Assessment (SIA) requirement and the Consent Clause in the Act have been diluted by various State laws. It needs to be mentioned that the LARR Act itself diluted the SIA requirement. Section 7(4):9 of the Act states that even if the SIA authority and the Expert Group reject a particular land acquisition, the government can proceed with the acquisition as long as “its reasons for doing so are recorded in writing”. It does not take much to imagine that this provision would have been regularly used. So, the edifice of SIA has been a façade right from the beginning. In case of the Consent Clause, the 2013 law does not make consent necessary for land acquired for government projects. Though many States have strict consent clauses, the LARR Act’s requirement is (usually) a higher percentage of the population accepting acquisition than what the State laws have stipulated. Right to eminent domain (that is, forcible acquisition of land/property for public good) is a right that most of the states have across the world; and one sees no reason to grudge it to the Indian state.
Because some people may not want to sell their land while others are willing, forcible acquisition is needed. What should be the relative percentage of ‘non-willing’ versus ‘willing’ could be stipulated by law but it is primarily a political issue. This is because even if the law is followed, the land-losers (say 15 per cent) may still not want to sell the land. The political party in power would have to use sincere efforts, excellent communication skills along with an acceptable compensation package to see a project through. If this is not happening, it is the duty of the Opposition party to raise a voice against injustice being committed. Admittedly, this is a somewhat rosy picture of democracy but a picture, nevertheless, towards which we should strive. Also, the ‘non-willing’ have a right to go to the courts and ask for redress under cases of forcible acquisitions.
The politics of presidential assent
The third issue is focussed on the President’s role. Presidential assent is not to be a formality as far as State laws under Article 254(2) are concerned. Based on a Supreme Court ruling, the President would need to engage in “active application of mind” before giving assent. This doesn’t necessarily imply that the President needs to reject the State laws, at least in this case.
The fact of the matter is that this is a peculiar case wherein the State legislatures and the Central government both want certain kinds of changes in the law. Besides, was this law was passed in 2013 with an eye to the forthcoming elections? If it were so, then it is a very dangerous precedent.Before the LARR Act was passed, the States had their own laws and the Land Acquisition Act, 1894, was hardly ever used. Even now, the States are free to pass their own laws and so the situation is back to square one. Needless to add, better-governed States will have less problems with respect to acquisitions and will stay the course on growth path. Other States will need to think hard.
Dhanmanjiri Sathe teaches Economics at Savitribai Phule Pune University.
करोड़ों की आबादी शौचालय से वंचित
स्वच्छ भारत अभियान में विविध प्रकार की संस्थाएं जागरूकता फैलाने के कार्य में लगी हैं। इसी क्रम में देश में स्वच्छता से जुड़ी कई रिपोर्ट आई हैं, उनमें ‘‘ओवरफ्लोइंग सिटीज’ विषयक अन्तरराष्ट्रीय चैरिटी नाम की संस्था की हालिया रिपोर्ट गौरतलब है। रिपोर्ट से साफ है कि भारत के नगरों के 10 करोड़ लोग अभी भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व के नगरों के प्रत्येक पांच में से एक के व्यक्ति के पास टॉयलट नहीं है। विश्व के शौचालयों से वंचित 70 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ भारत में हैं। इनमें से अधिकांश लोग जो टॉयलट प्रयोग करते भी हैं, तो वे भीड़भाड़ वाले सामुदायिक शौचालय हैं। उनमें से अधिकांश में साफ-सफाई नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से भी वे बहुत कमजोर स्थिति में हैं। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के ऐसे दस देशों में जहां लोग सुरक्षित और प्राइवेट टॉयलट से वंचित हैं, उनमें भारत के मुकाबले चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति ज्यादा खराब पाई गई है। शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अभी तक देश में 26 लाख से भी अधिक टॉयलट का निर्माण हो चुका है। अफसोस यह है कि अक्टूबर, 2019 तक पूरे होने वाले संपूर्ण अभियान का यह मात्र 40 फीसदी है। स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का सवाल है, तो उसके अन्तर्गत अभी 81 हजार टॉयलट का निर्माण करते हुए 32 फीसदी लक्ष्य ही पूर्ण हो पाया है। आंकड़े यह भी साफ करते हैं कि सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कहना न होगा कि नगरों में मात्र 23788 सार्वजनिक शौचालयों का ही निर्माण हो पाया है, जो अक्टूबर, 2019 के लक्ष्य का मात्र नौ फीसदी है। निश्चित ही भारत के नगरों में इस समय प्रत्येक क्षेत्र व घर के लिए स्वच्छ टॉयलट के निर्माण कराने की भारी चुनौती है। आंकड़े बताते हैं कि टॉयलट इत्यादि से जुड़ी स्वच्छता के कमजोर होने से डॉयरिया जैसी बीमारी से सालाना 3 लाख से अधिक बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं। घरों में टॉयलट न होने से महिलाओं व लड़कियों में असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ रही है। उन्हें शौच इत्यादि से निवृत्त होने के लिए सांयकाल या अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है। गांवों और नगरों में यौन हिंसा की होने वाली अधिकांश वारदात इसी का परिणाम ज्यादा हैं। गांव व नगरों की तमाम शिक्षण संस्थाओं में टॉयलट न होने से अधिकांश लड़कियां अपने शारीरिक परिवर्तन के कारण स्कूल जाने में हिचकती हैं। यही वजह है कि लड़कियों में ड्रॉपआउट रेट भी लगातार बढ़ रहा है। समुदायों के बीच कमजोर साफ-सफाई होने से चिकित्सा क्लिनिक भी कमजोर स्थिति में हैं। परिणाम है कि हेल्थ वर्कर और सेनिटेशन अभियान से जुड़े तमाम कर्मचरियों में संक्रमण वाले रोगों का जोखिम भी बढ़ रहा है। दरअसल, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्य मिशन शुरू होने तक देश में स्वच्छता को सार्वजानिक स्वास्य का महत्वपूर्ण अंग नहीं समझा गया। फिर भी मिशन ने प्रयास करके गांवों के घरों में शौचालयों के साथ में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराने का प्रयास किया। सच है कि चाहे घरों का शौचालय हो या सार्वजनिक, सभी में लगातार पानी की उपलब्धता के बिना काम नहीं चल सकता। यह भी कड़वा सच है कि इन शौचालयों का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता, जब तक इनकी साफ-सफाई ठीक से न हो। भारत में इस प्रकार की सुविधाओं के विस्तार के लिए धन की कोई खास व्यवस्था न होने के कारण इनका ठीक से कार्यान्वयन भी नहीं हो सका है।देखा जा रहा है कि सांस्कृतिक टैबू अभी भी अनेक घरों में शौचालयों के निर्माण में बाधा बने हुए हैं। स्वच्छता के मूल्यों का अभाव सभी के लिए स्वच्छता के मुद्दों के विस्तार को बाधित कर रहा है। स्वच्छता से जुड़े मुद्दों का सामाजीकरण न होने से स्वच्छता की जरूरत होने पर भी स्वच्छता कार्यक्रम नाकामी के कगार पर हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत में स्वच्छता से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे कार्यक्रम इस अभियान के कम सहायक होगे। यहां स्वच्छता से जुड़े विराट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में समूह व समुदाय के स्तर पर इच्छाशक्ति के साथ खड़े होकर शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ लोगों के मानसिक स्तर पर भी परिवर्तन लाने की महती आवश्कता है।
विशेष गुप्ता
Date: 22-11-16
धर्म की पहेली
धर्म और राष्ट्र दो ऐसी धारणाएं हैं, जिन पर लंबे समय से मनुष्य की मेधा उलझी हुई है। लगभग दो सदी से तो इनकी गुत्थी सुलझाने के लिए कितने ही दार्शनिकों, विचारकों, इतिहास-पुरु षों ने अलग-अलग तरह से व्याख्या करने की कोशिश की। लेकिन मानो किसी दुश्चक्र की तरह इनकी पहेली जहां-की-तहां खड़ी मिलती है। विडंबना देखिए कि आदर्श रूप में ये दोनों धारणाएं मनुष्य और उसके संसार को बेहतर बनाने का वादा करती हैं। मगर पिछली सदियों का इतिहास खगालें तो इन्हीं के नाम पर सबसे ज्यादा खून बहा है। इन दोनों का एक में मिल जाना तो भयंकर नतीजे लेकर आता है, जिसकी मिसालें बिखरी पड़ी हैं। इन्हीं को खून-खराबे, अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण, घोर अमानवीय व्यवहार, यहां तक कि व्यभिचार को जायज ठहराने का भी बहाना बनाया गया है। फिर भी, इनकी सत्ता बदस्तूर कायम है तो निश्चित रूप से कोई ऐसी डोर है, जिसके सहारे मानव मन इनकी ओर खिंचा चला जाता है। शायद इसी वजह से कार्ल मार्क्स ने धर्म को ‘‘अफीम’ कहा था। हाल में जारी आतंकवाद का तो एक पहलू धर्म ही है। मौजूदा दौर में दुनिया भर में और खासकर हमारे देश में भी धर्म के नाम पर तनाव का वातावरण पैदा होने लगा है। इसलिए प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की वह टिप्पणी खास अहमियत रखती है कि धर्म नितांत निजी मामला है। उन्होंने यह राय एक अन्य न्यायाधीश की किताब के विमोचन के दौरान जाहिर की। मतलब यह कि धर्म और आस्था को निजी मामला मानकर उसे राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। हमारा संविधान भी व्यक्ति की निजता की सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन सवाल तब उठता है जब किसी का धर्म दूसरे की आस्था के आड़े आ जाता है या उसके नाम पर किसी तरह का भेदभाव या अन्याय किया जाता है। इसमें भी एक सीमा रेखा अगर खींची जाए कि धर्म और आस्था को तो अलग रखा जाए मगर उसके नाम पर चलने वाली कुप्रथाएं मिटाने के लिए लोगों में एक जागरूकता पैदा की जाए तो बेहतर हो सकता है। कोशिश यह होनी चाहिए कि जिस समाज में जो बुराई या कुप्रथा व्याप्त है, उसके खिलाफ उसी समाज से आवाज उठे। किसी पर कुछ भी थोपने की प्रवृत्ति ही कट्टरता पैदा करती है, जिसके नतीजे हमेशा विनाश लेकर आते हैं। प्रधान न्यायाधीश इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि हर किसी की निजता का सम्मान किया जाए, वरना कट्टरता की धारा को बहने से रोकना नामुमकिन हो सकता है।
मराकश का मुकाम

अब जबकि मराकश सम्मेलन में दो सौ देशों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की प्रतिबद्धता जताई है तो पहली नजर में यह बड़ी खुशफहमी नजर आती है। सम्मेलन में प्रस्ताव पारित करके 2018 तक पेरिस जलवायु करार को लागू करने को हरी झंडी दे दी गई है। मगर इस नेक इरादे में पलीता लगाने वाले कई सारे मंजर भी सामने आए हैं। कुछ निहित स्वार्थों के चलते कृषि, वृत्त अनुकूलन जैसे मुद््दों पर चर्चा ही नहीं हुई। राजनीतिक आधार पर बंटे देशों की खींचतान कई बार साफ दिखाई दे जाती है। अमेरिका और चीन शुरू से अपनी चलाने की कोशिश करते देखे गए हैं। जिस हरित जलवायु कोष बनाने की बात हुई थी, उसमें अमेरिका को तीन सौ करोड़ डालर देने थे, लेकिन उसने अभी तक केवल पचास करोड़ डालर दिए हैं। मगर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान इस संधि से अपने देश को अलग करने का इरादा जता चुके हैं। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र में वीटो से लैस देशों में अतिराष्ट्रवादी ताकतों के उभार की वजह से भी आम सहमति को पलीता लग सकता है। सम्मेलन में भारत ने दोहा समझौते को लागू करने और विकसित देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन कम करने पर जोर दिया। बढ़ते तापमान की वजह से बाढ़, चक्रवाती तूफान और सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। इस सम्मेलन में विश्व मौसम संगठन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके मुताबिक आने वाले साल के बारे में नब्बे फीसद आशंका इस बात की बढ़ गई है कि गरमी के लिहाज से पिछला सारा रिकार्ड टूट जाएगा।
हालांकि मराकश सम्मेलन में देशों की भागीदारी उत्साह बढ़ाने वाली रही, और यह उम्मीद की जानी चाहिए कि विकसित देश अपनी घरेलू राजनीति या क्षुद्र भू-राजनीतिक इरादों को वैश्विक पर्यावरण की रक्षा में आड़े नहीं आने देंगे। जलवायु न किसी की इजारेदारी की चीज है और न ही निजी उपभोग की। कोई भी अव्यवस्था धरती के एक सिरे से दूसरे सिरे को डगमगा सकती है। कामना ही की जा सकती है कि पेरिस समझौता सौजन्यता और सख्यभाव से लागू हो जाएगा, जिसकी तरफ दुनिया पलक पसारे देख रही है।
Date: 22-11-16
लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सुझाव पर, कि लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए, सरकार ने गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है।

अगर लोकसभा और सारी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों, तो पहला लाभ यह होगा कि चुनाव के खर्चों में कमी आएगी। राज्यतंत्र पर जो वित्तीय भार पड़ता है वह भी कम होगा और राजनीतिक दलों को जो अलग-अलग चुनावों के लिए बार-बार चंदा जुटाना पड़ता है वह जहमत भी कुल मिलाकर कम होगी। दूसरा लाभ राजनीतिक स्थिरता के रूप में दिखेगा। पांच साल की अवधि में, उपचुनाव को छोड़ कर, और शायद स्थानीय निकायों के चुनावों को छोड़ कर, कोई चुनाव नहीं होंगे। राजनीतिक स्थिरता के फलस्वरूप विकास-कार्यों में तेजी आएगी। प्रशासन लोक शिकायतों के निवारण पर ज्यादा ध्यान दे सकेगा। जबकि जल्दी-जल्दी चुनाव के चलते थोड़े-थोड़े समय बाद किसी न किसी राज्य में, और कई बार कुछ राज्यों में एक साथ, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे विकास-कार्य बाधित होते हैं। ऐसे कई देश हैं जहां केंद्रीय और प्रांतीय चुनाव साथ-साथ होते हैं। मसलन, दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन में। लेकिन समस्या यह है कि एक साथ चुनाव का सुझाव तब तक अमल में नहीं आ सकता जब तक इसके लिए देश में राजनीतिक आम सहमति नहीं बनती, क्योंकि इसके लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा और संशोधन प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से पारित कराना होगा।
विधि मंत्रालय ने इसके कानूनी पहलुओं पर सोचना शुरू कर दिया है। संवैधानिक संशोधन की शर्त के अलावा एक अहम सवाल प्रबंध का भी है। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने हों, तब भी भारी सुरक्षा अमले की जरूरत पड़ती है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल का पिछला विधानसभा चुनाव छह चरणों में कराना पड़ा था। एक साथ चुनाव कराने के सुझाव पर निर्वाचन आयोग ने कोई सैद्धांतिक असहमति तो नहीं जताई है, पर व्यावहारिक चुनौतियां जरूर गिनाई हैं। जैसे, आयोग ने बताया है कि फिर कितनी बड़ी संख्या में नई वोटिंग मशीनें खरीदनी होंगी और दूसरे इंतजाम भी काफी करने होंगे। जब कुछ राज्यों के चुनाव कराने में ही सुरक्षा बलों का टोटा महसूस होता है, तो लोकसभा और सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर सुरक्षा संबंधी चुनौती कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक आम सहमति बनेगी तो इन परेशानियों का हल भी ढूंढ़ लिया जाएगा।