
22-07-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 22-07-25
At FTA’s heart, the promise of Global Capacity Centres
The United Kingdom-India Free Trade Agreement could be a catalyst for deeper engagement in the GCCs, a rapidly evolving ecosystem
Kishore Jayaraman, [ is OBE, India Chair, UK India Business Council (UKIBC) ]
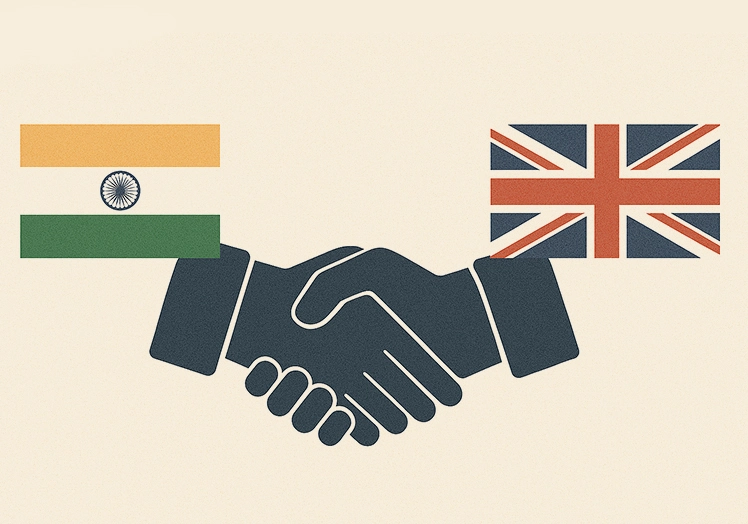
As the United Kingdom and India move steadily toward signing of their historic Free Trade Agreement (FTA), there is growing recognition of the FTA’s potential to redefine bilateral economic engagement. Among the most promising areas of collaboration is the rapidly evolving ecosystem of Global Capability Centres (GCCs) – a sector where India leads, and the U.K. can be a pivotal partner.
India is already home to more than 1,500 GCCs, employing over 1.9 million people and contributing significantly to the global innovation and digital transformation agendas of multinational corporations. Increasingly, British companies are looking to India not just as a cost-effective back office, but as a strategic partner for research and development, analytics, cybersecurity, and emerging tech solutions.
The FTA could be a catalyst for deeper engagement in this space. By easing regulatory barriers, facilitating smoother movement of professionals, and harmonising digital and data governance standards, the agreement can support the expansion of GCCs that serve U.K.-headquartered businesses – or leverage British expertise to serve global markets from India.
Much potential
The U.K’s Foreign Secretary David Lammy visited India within weeks of his taking office, demonstrating commitment towards the partnership with the U.K. The Business and Trade Secretary, Jonathan Reynolds’ visit ahead of resuming FTA negotiations, following suit. At the UK India Business Council (UKIBC), we think that there is real potential to further increase our trade, investment, and wider partnership. Prime Ministers Keir Starmer and Narendra Modi also had an extremely productive meeting at the G-20 Summit in Brazil, in 2024, agreeing to take the relationship to new heights.
From the U.K.’s perspective, the FTA is a timely opportunity to secure access to one of the world’s fastest-growing digital economies, while reinforcing its global services and innovation footprint post-Brexit. For India, greater U.K. investment and collaboration in the GCC space aligns perfectly with its digital economy ambitions, skilling objectives, and goal of becoming a global hub for high-value services.
The UKIBC has long championed the idea that the future of trade lies not just in goods but also in the services, skills and technology that power the new global economy. The GCCs stand at the intersection of all three.
The FTA can pave the way for easier cross-border collaboration, robust intellectual property frameworks, and smart mobility solutions that allow talent to move where it is most needed.
A well-crafted agreement can also address the practical challenges businesses face such as double taxation, data localisation mandates and misaligned standards, that often inhibit the scaling of GCCs. Addressing these through the FTA, or individually, will send a strong signal to investors and businesses in both nations.
According to a white paper released by Deloitte India, the country is making strides in the global GCC game, as India-based GCCs have emerged as strategic hubs for multinational companies to manage complex global tax operations, including corporate tax, indirect tax, transfer pricing, and litigation,
India’s current policy environment is highly conducive for GCC growth, even without a dedicated national GCC policy at the moment. The Ministry of Electronics and Information Technology (Meity) has formed an industry-led panel – including the National Association of Software and Services Companies (NASSCOM), Zinnov, KPMG, and Invest India – to design the national GCC framework outlined in Budget 2025. Its goal is to guide States in promoting GCCs, improving talent, infrastructure, innovation, and legal facilitation.
State government policies
Other than central government endeavours, we also see State governments rolling out landmark policies. Uttar Pradesh hosted its first “GCC Conclave” under Invest UP, bringing together policymakers and industry heavyweights (Microsoft, TCS, HCL, Standard Chartered). The event showcased U.P.’s infrastructure, incentives, and intent to host GCCs beyond National Capital Region cities, in Lucknow, Varanasi, Kanpur and Prayagraj.
In this context, the UKIBC recently held a closed-door consultation to bring together a distinguished group of leaders and experts to explore the expanding role of GCCs in driving innovation and economic growth in India. The group deliberated on a set of recommendations including global best practices from a governance perspective to help India achieve its economic ambitions set for GCCs. It also discussed these: whether there is a need for a dedicated national GCC policy now; whether organic growth from the past is best achieved in the absence of any such policies; or if having multiple State-level policies create unwanted competition instead of overall national progress. The need for honing talent diversity as well as skilfully managing the diversity of GCC’s themselves, was also underscored.
Some of the legal hurdles and the market outlook was touched upon, with some practical experiences of Indian and U.K. companies being shared. Additionally, the overall impact of India’s economic diplomacy efforts through FTAs on the Indian GCC ecosystem was touched on. These included aspects of how the U.K.-India FTA can be leveraged to help Indian GCCs climb up the global value chain, with a focus on talent diversity in terms of professional mobility across the two countries.
A knowledge corridor
As the two governments fine-tune the final provisions, industry leaders must continue to voice the importance of services, digital trade and mobility – the lifelines of modern commerce. GCCs, in particular, stand to gain from – and contribute to – this evolving partnership, shaping a resilient, knowledge-based corridor between the U.K. and India.
Date: 22-07-25
मौजूदा दौर में तकनीकी से ही आएगी आत्मनिर्भरता
संपादकीय
ऑटोमोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, एमआरआई मशीन से लेकर दर्जनों उत्पाद रेयर अर्थ तत्वों के बिना नहीं बन सकते। भारत में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है, लेकिन चीन से सस्ता मिल जाने के कारण इसे निकालने में निवेश नहीं किया जाता। पांचवें जनरेशन के स्टील्थ फाइटर्स के लिए हमें रूस, फ्रांस या अमेरिका का मुंह देखना होता है। हम खुश हुए जब अमेरिका की एक कंपनी ने इन जहाजों के इंजन बनाने में दिलचस्पी दिखाई। तेजस के लिए यही कंपनी एफ- 404 देने में दो साल पीछे चल रही है। इन जेट्स को बनाने में कौन विदेशी कंपनी सोर्स कोड देने को तैयार होगी, यह हमारे लिए अहम बात है। राफेल निर्माताओं ने तो मना कर दिया। लेकिन हम सोर्स कोड के मोहताज क्यों है? हमारी जरूरत की दवाओं के 70% मौलिक पदार्थों की सप्लाई चीन करता है। निजी दवा उद्योग चीनी माल से दवाएं बनाकर बेचने और निर्यात करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। क्या वजह है कि हम संसाधन और टैलेंट रहते हुए भी दूसरों के आसरे हैं? इसकी कुंजी है- शोध में निवेश । आज भारत अपनी 4 ट्रिलियन जीडीपी का मात्र 0.6% ही शोध में खर्च करता है, जबकि चीन इससे 30 गुना और अमेरिका 40 गुना कर रहा है। आज आत्म-निर्भरता केवल अनाज उत्पादन बढ़ाने से नहीं आएगी। तकनीकी और सामरिक आत्मनिर्भरता ज्यादा जरूरी है।
Date: 22-07-25
अमेरिका के साथ तालमेल रखना भारत के हित में है
मकरंद परांजपे, ( लेखक, चिंतक व भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के पूर्व निदेशक )
यह सच है कि भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अब परिपक्व हो चुके हैं। उन्हें अब शायद मुख्यधारा के मीडिया पेशेवरों से भी अधिक व्यू मिलने लगे हैं और वे लाखों दर्शकों को प्रभावित करते हैं। लेकिन इसमें एक खतरा है। अव्वल तो उनके हेडलाइंस बहुधा भ्रामक होते हैं। क्लिकनेट के लिए उनके शीर्षकों या थम्बनेल में अमूमन किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती का किसी अन्य दिग्गज का नाम शामिल होता है। वे हर हफ्ते, वीडियो-दर- वीडियो यह दावा करते हैं कि किसी ‘बड़े एक्शन’ की योजना बनाई जा रही है। और अगर ‘फिनफ्लुएंसर्स’ की बात करें तो वे अक्सर बाजार में किसी बड़े ‘क्रश’ का पूर्वानुमान लगाते हैं। जबकि उनकी भविष्यवाणियां शायद ही कभी सच होती हों।
हालांकि, सरकार समर्थित चैनलों में एक शगल आम है कि वे अपने प्रिय नेताओं को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू है। बड़े मानदंडों को लेकर नरमी से बोलने के बजाय हम छोटे मानकों पर कोलाहल का शिल्प रचने लगते हैं। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि आत्म-प्रवंचना हमें निश्चित ही उस गड्ढे में डाल देगी, जिसे हमने ही अपने लिए खोदा है। मैं यह कहकर अपने लिए आफत को न्योता दे रहा हूं लेकिन संभवत: अमेरिका को हमारी जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा आवश्यकता हमें अमेरिका की है।
वैश्विक भू-राजनीति में रणनीतिक तालमेल तो समझ आता है, पर रणनीतिक स्वायत्तता नहीं और आर्थिक सैन्य, तकनीकी, राजनीतिक, सांस्कृतिक हितों में अमेरिका के साथ तालमेल रखना भारत के हित में है। मैं फिर दोहराता हूं कि अराजकता, विघटन, सर्वसत्तावाद के खिलाफ आज लोकतंत्र ही सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण है। इसलिए दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों के नाते अमेरिका और भारत में स्वाभाविक साझेदारी निर्मित होती है। ऐसे में मसलन नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रम्प के प्रयासों का मखौल उड़ाने के बजाय हम इसका समर्थन कर सकते थे। हमें इससे क्या नुकसान होता? सच कहें तो हम इस खेल में पाकिस्तान से कहीं आगे निकल जाते। बेशक, व्यापार और तकनीकी लाभों के बदले ऐसा किया जा सकता था।
भारत को अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए व्यावहारिक गठबंधनों की जरूरत है, ऐसे में राष्ट्रवादी उत्साह के आवरण में प्रकट होने वाला हमारा अमेरिका-विरोध हमें अपने एक प्रमुख साझेदार से दूर कर सकता है। इंफ्लुएंसर्स का सनसनी फैलाने का जुनून गलत है, चाहे वह डॉलर की कीमत घटने को लेकर हो या फिर भारत की कथित भू-राजनीतिक जीत को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने को लेकर ऐसी अतिशयोक्तियों से एक विकृत वैश्विक दृष्टिकोण निर्मित होता है।
अमेरिका-विरोधी प्रोपगंडा का अधिकांश हिस्सा न केवल भ्रामक, बल्कि खतरनाक भी है। अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व में शीर्ष पर है। इसकी तुलना में हमारी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन पर है, जिसके 2025 में 4 ट्रिलियन के पार पहुंचने का अनुमान है। अमेरिकी रक्षा खर्च के आगे भारत का रक्षा खर्च बौना है और एआई से लेकर सेमीकंडक्टरों तक उसकी तकनीकी बढ़त से पार पाना तो हमारे लिए बेहद ही मुश्किल है। अमेरिका के बेस दुनियाभर में हैं। जमीन, समुद्र या अंतरिक्ष में उसकी क्षमताएं अतुलनीय हैं। यह दिखावा करना कि भारत अमेरिका के बिना भी चल सकता है, सच्चाई को नजरअंदाज करने जैसा है।
इंफ्लुएंसर्स के बीच डी-डॉलराइजेशन की कहानी खूब पसंद की जाती है। जबकि 2024 के स्विफ्ट डेटा के अनुसार डॉलर अभी भी वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में 60% हिस्सेदारी रखता है और 88% अंतरराष्ट्रीय लेन-देनों में काम आता है। इससे भी बढ़कर, अमेरिका-विरोध की दिखावटी बयानबाजी भारत-अमेरिका साझेदारी के स्पष्ट लाभों को भी अकसर अनदेखा कर देती है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी वाला ‘क्वाड’ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए भारतीय रणनीति का प्रमुख आधार है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और हमारा द्विपक्षीय व्यापार 190 अरब डॉलर से अधिक है। ऐपल और टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, जिससे नौकरियां पैदा हो रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिका या उसके नेताओं का मजाक उड़ाना इस साझेदारी को खतरे में डालता है, जो भारत की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
Date: 22-07-25
सांसद अपनी भी समीक्षा करें
आशुतोष झा, ( लेखक दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक हैं )
संविधान, लोकतंत्र तो कुछ अरसे से राजनीति में चर्चा के केंद्र में हैं ही, लेकिन वक्त आ गया है कि अब विधायिका पर भी चर्चा हो और इसका ठोस आकलन हो कि संसद जन आकांक्षाओं को पूरा कर पा रही है या नहीं? यदि नहीं तो इसके लिए उत्तरदायी कौन हैं, कितना हैं और क्यों हैं? संसद सही तरह से तब काम करेगी, जब पक्ष-विपक्षी के दल यानी सांसद अपना काम ठीक से करेंगे। संसद के सदस्यों को कैसे जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, एक स्वतंत्र एजेंसी इसका पूरा अध्ययन कर जनता के सामने रख दे कि किसे जिम्मेदार माना जाए? संसदीय परंपरा, नियम-कानून की कसौटी पर यह अध्ययन हो और उसे सार्वजनिक किया जाए। यह इसलिए जरूरी हो गया है, क्योंकि साल दर साल संसद की कार्यवाही चलाने के बजाय रोकने की कवायद तेज होने लगी हैं। बहस की गुणवत्ता के बजाय शोर के जोर से सफलता आंकी जाने लगी है। जनता के असल मुद्दों के बजाय आमतौर पर सतही राजनीतिक और चुनावी मुद्दे हावी होने लगे हैं। याद कीजिए कि किसी संसदीय सत्र से पहले ऐसी खबर पढ़ी क्या कि सत्र बहुत फलदायक होने वाला है…। यह खबर हर बार पढ़ी होगी कि हंगामेदार रहेगी। आरोप-प्रत्यारोप इस पर चलता है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार विधेयक लेकर आती है। विपक्ष के पास पूरा अधिकार होता है कि उन पर अपने विचार रखे, लेकिन विपक्ष का एजेंडा तय करता है कि सदन की कार्यवाही चल पाएगी या नहीं?
राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में थोड़ी भी रुचि रखने और दलगत राजनीतिक हित से अधिक देश की चिंता करने वाले किसी जागरूक नागरिक से यदि पूछा जाए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव रुकवाने का जो दावा किया गया, उस पर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार का क्या कहना है ? जवाब यही आएगा कि प्रधानमंत्री ने उस दावे को कड़ाई से तब खारिज कर दिया था, जब वह कनाडा गए थे और वहां से ट्रंप पर फोन से बात की थी। आपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों में गए संसदीय प्रतिनिधिमंडल में सब दलों के सांसदों ने वैश्विक मंच पर क्या कहा, सबको पता है। इन प्रतिनिधिमंडलों में कांग्रेस के भी कई सांसद थे। आखिर संसद में विपक्ष क्या जानना चाहता है? ट्रंप के बड़बोलेपन से दुनिया परेशान है। जिन देशों के साथ वह व्यापार समझौते की घोषणा कर रहे हैं, वे अचंभित हैं, लेकिन हमारे तमाम विपक्षी सांसद हैं कि उन्हें ट्रंप के बड़बोले बयानों और बेतुके दावों पर चर्चा करनी हैं। आपरेशन सिंदूर में सेना की वीरता पर देश का सीना गर्व से चौड़ा है। संसद में बहस करना चाहें तो कर लें, लेकिन क्या सेना की रणनीति पर चर्चा करेंगे या सेना को यह बताने की कोशिश करेंगे कि सैन्य रणनीति कैसे बनाई जाती है ? ऐसे मुद्दों पर संसदीय स्थायी समिति में खुलकर बात हो सकती हैं, लेकिन जोर सदन में चर्चा का है।
बिहार में चुनाव आयोग की और से चल रहा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पहली सुनवाई में कोर्ट ने रोक लगाने से इन्कार कर दिया और संभवतः अगले सप्ताह फैसला आ सकता है। फिर चर्चा किस चीज पर ? फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकार को माना है और केवल समय को लेकर और नागरिकता तय करने के संदर्भ में सवाल उठाया है। सदन में जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन उस चर्चा का सार्थक होना भी जरूरी है, खासकर तब जब संसद साल में बमुश्किल 40-50 दिन ही सुचारु रूप से चल पाती है।
राजनीतिक दलों की ओर से मांग की जाती रही है कि साल में कम से कम सौ दिन सत्र चलना चाहिए, लेकिन अब इस मांग की ईमानदारी पर भरोसा नहीं होता। चाहें तो सदस्यों की उपस्थिति का रजिस्टर देख लें। क्या वक्त नहीं आ गया है कि सदस्यों की उपस्थिति को जरूरी किया जाए। कुछ देशों में ऐसे नियम हैं। अवरोध कम करने के लिए कुछ वर्षों से राज्यसभा में प्रश्नकाल से पहले शून्यकाल कर दिया गया है। इसका थोड़ा सकारात्मक असर दिखा हैं। लोकसभा में भी इस पर विचार होना चाहिए। इसके भी ठोस नियम बनने चाहिए कि सप्ताह में चार दिन केवल सूचीबद्ध विषयों पर ही कार्यवाही चलेगी। संसदीय अराजकता और मनमानी को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। संसद को सही तरह चलना ही होगा।
कई विधानसभाएं ऐसी हैं, जो साल में 30 दिन भी नहीं चलती हैं, जबकि संविधान में अधिकतम छह महीने में सत्र बुलाने की बाध्यता है। कुछ समय पहले तक दिल्ली में तो विधानसभा को राजनीतिक मंच बना दिया गया था। यहां आम आदमी पार्टी की सरकार कवच ओढ़कर मोदी सरकार पर मनचाहे आरोप लगाती थी, क्योंकि विधायी सदन में की गई टिप्पणियों पर कोर्ट में केस नहीं किए जा सकते। दो दिन के सत्र बुलाए जाते थे, फिर रोक दिए जाते थे। फिर इच्छा के अनुसार सत्र आहूत कर लिया जाता था। जिस विधायी सदन में बहुमत के लिए राजनीतिक दल कमर कसे खड़े होते हैं, उसे प्रासंगिक बनाने, सुचारु रूप से चलाने में किसी की रुचि नहीं दिखती। सरकार के लिए विधेयक अहम हैं। कई बार तो यह सुविधाजनक भी होता है कि अवरोध में ही विधेयक पारित करा लिए जाएं, लेकिन सवाल विपक्ष का है कि वह सरकार के मुफीद ऐस माहौल बनाता ही क्यों है?
इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण होता है हर दो-तीन महीने में होने वाले चुनाव | ऐसे में सबको वही मुद्दे चाहिए, जो गर्मी पैदा कर सकें। ब्रेकिंग न्यूज बना सकें। आरोप-प्रत्यारोप का मंच दे सकें। क्या मान लेना चाहिए कि संसद तभी सुचारु ढंग से चल पाएगी और प्रासंगिक हो पाएगी, जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं? एक साथ चुनाव कई मर्ज की दवा साबित हो सकता है। तब गृह मंत्रालय के पास भी एनआरसी को पूरा करने का वक्त होगा और चुनाव आयोग के पास मौका होगा कि उसके आधार पर मतदाताओं की सूची दुरुस्त कर ले।
Date: 22-07-25
सामने आते अतीत के अनछुए पहलू
डा. विनोद यादव, ( लेखक इतिहासकार हैं )
पिछले कुछ महीनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तिलवाड़ा साकिन, हरियाणा के टोपरा कलां और राजस्थान के बहज नामक पुरातत्व स्थलों से ताम्रयुगीन, महाभारतकालीन, मौर्यकाल, शुंग काल और कुषाण काल के अनेक महत्वपूर्ण पुरावशेष मिले हैं। तिलवाड़ा साकिन गांव में हुए उत्खनन से 4,000 साल पुराने रथ का पहिया मिला है, जो तांबे की परत से ढका हुआ है। 1900 से 1500 ईसा पूर्व के तांबे की कटारें, तलवारें, औजार मिले हैं। तिलवाड़ा साकिन से केवल 10 किमी दूर सिनौली गांव से भी तांबे की परत चढ़े तीन युद्ध रथ और अति दुर्लभ लकड़ी के ताबूत में संरक्षित किए गए आठ मानव कंकाल, युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले कवच, हेलमेट, तांबे की तलवारें खंजर, स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं। सिनौली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने सर्वप्रथम 2005 में उत्खनन कार्य कराया था। तब पुरातत्वविदों को यहां से करीब 116 मानव कंकाल, स्वर्णनिधि ( बड़ी संख्या में सोने के कंगन, सोने के मनके और सोने की मानवाकृति) प्राप्त हुई थी।
तिलवाड़ा साकिन और सिनौली में मिले पुरावशेषों में एकरूपता की झलक मिलती हैं। यह पूरा परिक्षेत्र कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर के अंतर्गत आता था। तिलवाड़ा और सिनौली की खुदाई में जो बर्तन और दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं, वे महाभारत, रामायण और वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कथाओं से मेल खाते हैं। दोनों स्थलों से मिले मृदभांड और तांबे के बर्तनों की संरचना, नक्काशी और आकार एक जैसा है। इन दोनों स्थलों से मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग भी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी योद्धा जनजातियों में से एक यहां निवास कर रही थी । ये लोग प्रवासी नहीं, बल्कि हड़प्पा सभ्यता से अलग संस्कृति वाले स्वदेशी योद्धा थे। इससे यह भी पता चलता है कि वैदिक युग के लोग बहुत कुशल कारीगर थे। उन्हें धातु पिघलाना, उसे ढालना और लकड़ी पर तांबे की परत चढ़ाना अच्छी तरह आता था । महिलाओं के कंकालों के साथ मिली तलवारें और अन्य पुरावशेष इस बात के सुबूत देते हैं कि प्राचीन भारत में महिलाओं की सामाजिक हैसियत पुरुषों के बराबर थी। गंगा-यमुना दोआब में स्थित पुरातात्विक स्थलों से मिले ये पुरावशेष वामपंथी इतिहासकारों के फैलाए उस झूठ की पोल खोलते हैं कि आर्य विदेशी आक्रमणकारी थे और वे अपने साथ रथ और हथियार लेकर आए। ये पुरावशेष आर्यों के भारतीय होने के सिद्धांत को पुख्ता करते हैं।
चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में आज के हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित सुघ नामक गंव के बौद्ध विहार का बहुत सुंदर वर्णन किया है। सुध गांव के प्राचीन टीले पर सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए पुरावशेष आज भी मौजूद हैं। हाल में हरियाणा सरकार ने राज्य में 28 बौद्ध स्तूप निर्मित किए जाने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत यमुनानगर के ऐतिहासिक गांव टोपरा कलां में भगवान बुद्ध के स्तूप निर्माण के साथ होगी। वर्तमान में टोपरा गांव प्राचीन टीले पर स्थापित है और मौर्य युग के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों को यहां आसानी से देखा जा सकता है। हाल में आइआइटी, कानपुर के शोधकर्ताओं ने पुरातात्विक अवशेषों का पता लगाने की अत्याधुनिक तकनीक ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ( जीपीआर) द्वारा टोपरा कलां गांव के टीले का गहन सर्वेक्षण किया। इसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय तरंगों को जमीन के भीतर भेजा गया। इस तकनीक द्वारा शोधकर्ताओं को छह से सात फीट की गहराई पर स्तूप जैसी अर्ध गोलाकार संरचनाओं, ईंट की दीवारों और आवासीय कक्षों जैसे पैटर्न बने होने के संकेत मिले। शोधकर्ताओं की टीम ने एक और दिलचस्प जगह का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण किया, जिसे स्थानीय लोग ‘जरासंध का किला’ कहते हैं, यहां भी दीवारनुमा संरचना होने के संकेत मिले हैं। पुरातात्विक उत्खनन की इसी कड़ी में एएसआइ को राजस्थान के डीग जिले के बहज गांव में भी 3500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। खोदाई के दौरान शोधकर्ताओं को गांव में 23 मीटर की गहराई पर एक प्राचीन नदी तंत्र मिला। इतिहासकार इसे ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी से जोड़कर देख रहे हैं। इसके साथ ही मिट्टी के खंभों से बनी इमारतों के पुरावशेष परतदार दीवार वाली खंदकें और भट्ठियां भी मिली हैं। 15 हवन कुंड, शिव-पार्वती की टेराकोटा मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। यहां जो ब्राह्मी लिपि की मोहरें मिली हैं, वे भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक के सबसे पुराने साक्ष्य हैं। मथुरा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहज गांव सरस्वती बेसिन की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने वाली कड़ी है।
कुल मिलाकर खोदाई में मिले ये पुरावशेष साफ-साफ बता रहे हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास की समझ सामान्य बोध से अधिक पुरानी और विस्तृत हैं। बस जरूरत हैं तो तमाम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर भारत के गौरवशाली अतीत को नए नजरिए से देखने की । यह खोज न केवल इन क्षेत्रों की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई दे रही हैं, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के उन अनछुए अध्यायों को फिर से खोलने और नए सिरे लिखने का अवसर भी दे रही हैं जिन्हें साजिश के तहत दबा दिया गया है।

Date: 22-07-25
नवाचार के लिए सही फर्मों का चयन अहम
नौशाद फोर्ब्स

हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शोध, विकास एवं नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत देश के उद्योग जगत को 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन करने की बात कही गई है। इसमें से 20,000 करोड़ रुपये की राशि इस वर्ष के बजट में तय है। यह फंड किस प्रकार वितरित किया जाएगा, इसे लेकर आरंभिक टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि इसका बड़ा हिस्सा कम ब्याज या शून्य ब्याज दर पर कई फंड ऑफ फंड्स और सीधे कंपनियों को दिया जाएगा। यहां जब मैं फंड ऑफ फंड्स सुनता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। मुझे नहीं पता है कि सीधे नवाचार बढ़ाने के लिए उन्हें कैसे जवाबदेह बनाया जाएगा। मेरा मानना है कि ज्यादातर धनराशि सीधे कंपनियों को दी जानी चाहिए। सवाल यह है कि कंपनियों को क्यों ? किन कंपनियों को और कैसे वित्तीय मदद दी जाए ?
फर्मों को धन क्यों
नवाचार कंपनियों में होता है। इसमें कुछ किंतु परंतु हो सकता है पर यह तथ्य सही है। आप बाकी सब कुछ सही कर लें उच्च शिक्षा में सार्वजनिक धन वाले शोध को सही ढंग से अंजाम दें, राष्ट्रीय मिशन को सही ढंग से आगे ले जाएं, धनराशि को बिना लालफीताशाही के तेज गति से आने दें लेकिन कपंनियों में जो हो रहा है उसे गलत समझ लें, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं इस बात पर जितना जोर दूं कम है दुनिया भर में नवाचार मुख्यतः फर्मों में ही होता है। केंद्रीय नवाचार गतिविधियां मसलन बाजार की तलाश, डिजाइन और वितरण का काम सभी कंपनियों में होता है। शोध और नए ज्ञान अमूल्य हो सकते हैं लेकिन वे नवाचार में सिर्फ उपयोग होते हैं, वे उसका मूल नहीं होते कंपनियों को शोध एवं विकास में अधिक निवेश के लिए प्रेरित करना, उस शोध एवं विकास को नवीन उत्पादों और सेवाओं में परिवर्तित करना, तथा स्वामित्व प्रौद्योगिकी के इर्द-गिर्द व्यवसाय का निर्माण करना, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सके, एक जीवंत राष्ट्रीय नवाचार प्रणाली की कुंजी है।
ऐसे में कंपनियों को ऐसी किसी भी योजना के केंद्र में होना चाहिए जो नवाचार को बढ़ाना चाहती है। कंपनियों में शोध एवं विकास की सही व्यवस्था सार्वजनिक शोध को जिस प्रकार आकर्षित कर सकती है। वैसा कोई और व्यवस्था नहीं कर सकती है। परंतु भारतीय उद्योग द्वारा शोध एवं विकास में अपर्याप्त निवेश करना ही हमारे नवाचार को प्रभावित कर रहा है। आरडीआई योजना को इस पर ध्यान देना चाहिए और यह काम फंड ऑफ फंड्स जैसे बिचौलियों के बिना करना चाहिए
धनराशि क्षमता पर निर्भर हो
तथ्यों से शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने इस स्तंभ में पहले और अपनी किताब में भी कहा है और हर मिलने वाले से कहता हूं, भारतीय उद्योग जगत शोध एवं विकास में बहुत कम निवेश करता है। हम अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का महज़ 0.3 फीसदी आंतरिक शोध एवं विकास में लगाते हं जबकि वैश्विक औसत 15 फीसदी है। हमारी 10 सबसे कामयाब गैर वित्तीय कंपनियां (रिफाइनिंग, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की उच्च मुनाफा कमाने वाली कंपनियां) अपने मुनाफे का 2 फीसदी शोध एवं विकास पर व्यय करती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी में सफल कंपनियां मुनाफे का 29 से 55 फीसदी शोध एवं विकास में लगाती हैं। यूं ही नहीं, दुनिया के शीर्ष 10 प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां नदारद हैं। लब्बोलुआब यह है कि देश के उद्योग जगत का अधिकांश हिस्सा इतना शोध एवं विकास कार्य नहीं कर रहा है कि फंडिंग में जो इजाफा हो रहा है उसकी तत्काल खपत कर सके। 20,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन अच्छी खासी राशि है। शोध एवं विकास व्यय मोटे तौर पर लोगों पर है- औसतन उपकरण और सामग्री पर कुल व्यय का एक तिहाई से भी कम खर्च होता है। लगभग 20,000 करोड़ रुपये के व्यय से शोध एवं विकास में लगभग 20,000 और लोगों को जोड़ा जा सकता है। इनमें से कौन सी कंपनियां एक वर्ष में बड़े पैमाने पर विस्तार कर पाएंगी ?
हमें ऐसी कंपनियों की आवश्यकता है जो शोध एवं विकास में अच्छी खासी राशि का निवेश कर रही हों और अंतरराष्ट्रीय स्तर का शोध एवं विकास करें। हमें ऐसी कंपनियां चुननी होगी जो पहले ही शोध एवं विकास के क्षेत्र में अच्छा खासा काम कर रही हों। मिसाल के तौर पर उनकी शोध एवं विकास तीव्रता (बिक्री के प्रतिशत के रूप में शोध एवं विकास) उनके अंतरराष्ट्रीय समकक्षों की कम से कम आधी हो । दुनिया की शीर्ष 2,500 कंपनियों और हमारे देश की कंपनियों के बारे में यह आंकड़ा आसानी से उपलब्ध है। आंकड़े बताते हैं कि छह क्षेत्रों यानी औषधि, रसायन, ऑटो, डिफेंस, औद्योगिक इंजीनियरिंग और खाद्य क्षेत्र की हमारी शीर्ष पांच कंपनियों में औसतन शोध एवं विकास तीव्रता वैश्विक समकक्षों की आधी से ज्यादा है। इन क्षेत्रों में शोध एवं विकास में सबसे अधिक निवेश करने वाली कंपनियों में अपना शोध एवं विकास टीम बढ़ाने की सबसे अधिक क्षमता होनी चाहिए। एक उदार सीधी फंडिंग योजना से सामान्य फंड की उपलब्धता की तुलना में अधिक आवेदन आने चाहिए। भारत के शीर्ष 300 शोध एवं विकास निवेशकों में से कई आवेदन कर सकते हैं। हमारी 100वीं सबसे अधिक खर्च करने वाली कंपनी ने वर्ष 2022-23 में शोध एवं विकास में करीब 97 करोड़ रुपये का निवेश किया। हमारी 200वीं सबसे अधिक खर्च करने वाली कंपनी ने करीब 33 करोड़ रुपये और 300वीं बड़ी कंपनी ने करीब 16 करोड़ रुपये का निवेश किया। दुनिया की शीर्ष कंपनियों की तुलना में यह बेहद कम है। आरडीआई योजना से इसे बदलने का प्रयास करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि हम जिन कंपनियों को आरडीआई द्वारा वित्त पोषित करते हैं, उन्हें यह कहना चाहिए कि वे अगले 12 महीनों में शोध एवं विकास के काम में लगाए जाने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाकर डेढ़ गुना करें। यदि हम ऐसा कामयाबी से कर लेते हैं तो यह सिलसिला जारी रखा जा सकता है। पांच साल में निरंतर सफल कंपनियां मौजूदा शोध एवं विकास निवेश को आठ गुना तक बढ़ाना होगा। इससे देश में एक मजबूत शोध एवं विकास परंपरा तैयार हो जाएगी और नए उत्पाद और सेवाएं दुनिया के सामने आने शुरू हो जाएंगी। एक दूसरी आवश्यकता भी है। जिन कंपनियों को आरडीआई की फंडिंग मिले उन्हें मौजूदा शोध एवं विकास में और गहराई लानी चाहिए। गहराई से तात्पर्य है कि उन्हें कम प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) में अधिक निवेश करना चाहिए। कंपनियों को अपने नवाचार के प्रयोगों को गहराई प्रदान करने के लिए सार्वजनिक फंडिंग वाले शोध का इस्तेमाल करना चाहिए।
कैसा दिखता है भविष्य
आज हमारे पास ऐसी एक भी कंपनी नहीं है जो टर्नओवर के प्रतिशत के मामले में या शोध एवं विकास पर कुल खर्च की जाने वाली राशि के मामले में अपनी वैश्विक समकक्ष कंपनियों का मुकाबला कर सके। पांच साल बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि तकरीबन 100 से अधिक भारतीय कंपनियां ऐसा करती हुई नजर आएंगी। ये कंपनियां अन्य अनेक कंपनियों के लिए रोल मॉडल का काम करेंगी और इस तरह हम एक जीवंत राष्ट्रीय नवाचार प्रणाली तैयार कर सकेंगे।