
21-08-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:21-08-20
Date:21-08-20
One Cheer
Creation of NRA is a positive step but real reform will step up job creation
TOI Editorials
Making good a Budget promise, the Union Cabinet on Wednesday approved the creation of the National Recruitment Agency (NRA). The NRA will encompass the role of three independent agencies and conduct a nationwide preliminary test for non-technical jobs (Groups B and C) in the government, Railways and banks. The underlying idea is to use advances in communications technology to conduct a common eligibility test (CET). This addresses two challenges. It allows conducting the preliminary test in a geographically dispersed manner, and reduces the number of tests aspirants take.
This is undoubtedly an important step in making life simpler for millions of job aspirants, while lowering associated costs as the CET score can be used for multiple jobs. About 25-30 million candidates take these tests, which makes the creation of NRA a praiseworthy move. Another benefit is that it minimises the risk of malpractices which crop up in the current system. NRA has also been charged with another important task, to help aspirants prepare through mock tests. If this objective is carried out efficiently it will be of immense help to poorer job aspirants.
Jitendra Singh, the junior minister in the PMO, referred to the creation of NRA as a “revolutionary reform”. That is far fetched. The development has to be located in a larger context. A mere 1.25 lakh vacancies are available, which means that up to 240 aspirants compete for each job. From the standpoint of the national economy, these jobs are not the most productive ones. The sheer number who apply is a pointer to the lack of adequate alternatives. Enthusiasm for NRA, unfortunately, also shows up the shortcomings in our economic policy.
CMIE this week provided an update on the employment situation after four months of lockdown. It is worrisome. The economy has witnessed a contraction in salaried jobs and a growth in informal sector jobs. This suggests that the quality of jobs has deteriorated. This can only put more pressure on the aspirant for the non-technical posts that the government fills. The government cannot solve India’s jobs crisis directly. Genuinely revolutionary reform will come when the government creates an enabling environment that offers millions of aspirants for government jobs better alternatives in the private sector. That requires policies to unleash India’s entrepreneurial potential and rouse ‘animal spirits’. NRA is a positive step but not a revolutionary one.
Date:21-08-20
Make In India, For The World
To grow rich is glorious: How India can return to its past as a great trading power
Ajay Srivastava , [ The writer is an Indian Trade Service officer. ]
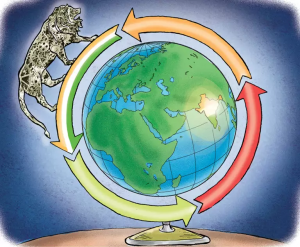
In his Independence Day speech, Prime Minister Narendra Modi repositioned the Make in India agenda as ‘Make in India for the world’. This signifies India’s aspiration to be a powerful trading nation on the back of quality products, competitive manufacturing, and integration into the world economy.
A robust trading nation is in a better position to set the agenda and influence narratives. Let us understand why trade is good and how we can be a powerful trading nation.
Almost everyone now agrees that trade is good for countries. We owe this understanding to David Ricardo, who in 1817 provided the foolproof argument in support of trade. His theory of comparative advantage says all countries gain from trade even when one country’s workers are more efficient at producing every single product than workers in other countries.
But how could this be possible? Ricardo used the following example to prove his point. Let’s say the world has only two countries, Portugal and England. Each produces only two goods, cloth and wine. The quality of produce in both countries is the same. In England, it takes 100 hours of labour to produce one piece of cloth and 120 hours to produce one litre of wine. So it takes a total of 220 hours to produce one piece of cloth and one litre of wine.
In Portugal, it takes 90 hours to produce one piece of cloth and 80 hours to produce one litre of wine. Portugal is more efficient than England in making both cloth and wine. We say Portugal has an absolute advantage in making both products. Should Portugal produce both?
Let us say both countries decide to produce only one item in which it is more efficient and buy the other. England decides to produce cloth as making one piece of cloth takes fewer hours than making one litre of wine. Portugal chooses wine for similar reasons.
A small calculation shows that in 220 hours, England will produce 2.2 pieces of cloth (100 hours for making one piece) and Portugal 2.125 litre of wine (80 hours to make one litre of wine). Now England sells one piece of cloth to Portugal for one litre of wine. After consuming one piece of cloth, England is still left with a surplus of 0.2 pieces of cloth. Portugal, after consuming one litre of wine, still had an excess of 0.125 litre of wine. Both the countries now have a surplus, and trade has created this surplus.
The above example shows the two countries are better off when they trade than when they produce and consume everything. In a testimony to the truth of Ricardo’s theory, trade expanded 6,000 times in the past 200 years.
But free trade principles work only as long as everyone plays by the book. The delicate balance is distorted when some countries take liberty with the globally agreed rules. For example, China uses a combination of massive subsidies and intellectual property theft, to become the dominant producer and exporter of many essential products.
For solar panels alone, China used to give an annual subsidy exceeding $15 billion. Local manufacturing in most countries could not compete with cheap imports from China, and died. China also uses the third country FTA route to sell subsidised products. For example, it’s alleged Chinese steel firms based in Indonesia export subsidised steel products to India using the low duty benefit under the India-Asean FTA. The comparative advantage theory goes for a toss, if products from one country become competitive because of massive subsidies.
How should India promote its manufacturing and trade? A fourfold plan will help.
First, reduce input costs. High duties on raw materials, expensive credit, erratic power supply, time taking land transactions, delay in refund of taxes, and less productive labour increase the input cost. Deep reforms in these areas will make India an attractive place to do business.
Second, define ‘Make in India for the world’ standards and make it a quality label. This will require setting up a large number of design studios, innovation labs, and strengthening of standards and quality infrastructure. MSMEs should have free access to such resources.
Third, expand manufacturing and trade of the products the world buys most – electronics, organic chemicals, machinery, apparel, telecom etc. We must avoid becoming a hub for superficial assembly of imported components. It makes us critically dependent on a few supplier countries. We have a better model. Nokia in 2007, while setting up mobile phone manufacturing facilities in Tamil Nadu, collocated most component manufacturers. This ensured high domestic value addition.
So a better alternative is becoming a component manufacturing hub. But this requires deep expertise, which currently we do not have for most components. We need joint ventures and external investments. Countries use attractive sectoral packages to get investment in scale manufacturing and promote global value chain participation. India will also need reforms in import duty structure, building efficient ports, and online systems.
Finally, avoid critical dependence on any country. We need to develop self-sufficiency in bulk drugs/ APIs, power equipment, everyday use goods, and defence related products etc. We should be willing to pay the additional price for this.
Becoming a great trading power would require participation of business and technology experts and not mere economists and bureaucrats. It will transform our agriculture, manufacturing, technology, logistics, education, and most other sectors.
Empower Municipal Bodies, Rainproof Towns
ET Editorials
The rainy season has now become synonymous with urban dysfunction. Rains over the past few days in the National Capital Region have caused flooding and waterlogging, and impeded mobility. This is not just Delhi’s story. Urban flooding is now a regular occurrence elsewhere, too. India cannot be a leading economy of the world with its cities flooding come every shower. The fix lies in urban planning and governance. Building better for greater resilience is one pillar of this effort.
That translates to improved planning to build infrastructure that is resilient and adaptive to climate change. Improved planning and administration would require strict adherence to norms, rules-based systems that dispense with perpetual ad-hocism. The second pillar is improved urban governance. For far too long, the urban authorities have failed to deliver on their basic responsibility to maintain the city’s systems — drainage, lighting, roads, mobility. Municipal bodies must be empowered to make decisions, have the requisite personnel and finances to keep the city in proper running condition. These bodies also need to ensure they draw on all available expertise to build and retrofit their cities to meet the challenges posed by threats such as climate change. Once so empowered, local urban authorities must be held accountable for the state of their city.
Municipalities need a proper fiscal base and the political will to make use of the base. Property tax is the most logical and lucrative source of tax. The better the governance, the more valuable the property. Municipalities can issue bonds on the strength of this fiscal base to raise the resources they need to invest in urban systems and infrastructure. Property owners and local politicians must accept that there are no free lunches.
A new social contract
We need to fundamentally reform our labour markets, attract people to cities where we ensure healthy living conditions, and create economic opportunities in rural India.
Naushad Forbes , [ The writer is former President CII, Chairman India@75 Foundation and co-Chairman of Forbes Marshall.]
A well-known saying attributed to the Chinese sage Confucious is “may you live in interesting times”. What is less well known is that Confucious meant this as a curse — interesting times remove time for reflection and make us think about our baser instincts. We live in far too interesting a time: An unprecedented and worsening health crisis, and the knock-on effect of the worst economic performance in our independent history. So let us rise above Confucious and reflect on where we must be as a country when India turns 75 in 2022.
The Prime Minister, while addressing the Confederation of Indian Industry (CII) annual meeting this year, urged those present to think big and partner with the government in putting India on the path to growth. This is an important call. There is much that we can achieve if government and industry work towards the same objective, and in a spirit of mutual trust.
Employment is one such area. Over 85 per cent of employment in India is in the informal sector. An unplanned national lockdown halted economic activity and wiped out livelihoods, especially of informal workers. The Centre for Monitoring the Indian Economy (CMIE) estimates that between mid-March and mid-April, 120 million people lost their jobs, with unemployment rising to an all-time high of 27 per cent. Left with nothing, we saw reverse migration on an unprecedented scale — some 10 million people abandoned cities to return to their native villages. For a while, our media was full of discussion of the need to address some of our most chronic social problems.
In the last two months, things have improved. CMIE reports that unemployment is now down to around 9 per cent, and as economic activity has restarted in cities, labour has begun returning from villages. As things have returned to normal, the priority for addressing our most chronic social problems has reduced. We must not waste this crisis. There are three problems we must address: Labour regulation, living conditions for migrant labour in cities, and the strength of our rural economy.
Labour regulation must start with a clear-eyed recognition of facts: We have stringent labour laws to protect workers, but this covers only the formal sector — under 15 per cent of employment. This “labour aristocracy” has almost complete protection, and employers have almost no flexibility. The 85 per cent of our workforce who are informally employed, meanwhile, have almost no protection, and employers have almost complete flexibility. We need to address both ends of the labour spectrum to get the balance right between flexibility and protection for all labour. Everyone must have a minimum level of protection, and every employer a minimum level of flexibility. This calls for a new social contract to define a well-calibrated social security system. This huge project demands good faith and strong leadership by industry, labour and government. It will take years to get it right, but if we don’t fix our employment system now when this issue has achieved such prominence, we will always regret the missed opportunity.
Living conditions in our cities is the second challenge. For too long, we have been content to drive by slums where some of the people who clean our homes, deliver our goods, and repair our equipment live in squalor. How do we set in force a massive private home-building programme? It probably needs much more liberal land-use regulations — our cities have among the least generous floor-space indices (FSI) in the world. New York, Hong Kong, and Tokyo have an FSI five times Mumbai’s. If five times as many people can live in the same area, it would drastically reduce rents for quality housing in our cities. Again, this is a multi-year project, and it involves state and city governments partnering with private developers. India is unique in having 70 per cent of our population still residing in rural areas. Seventy-three years after Independence, this is a statement of failed development. We must encourage the migration of people to higher productivity occupations in our cities. And we must ensure that clean, affordable and accessible housing is available for all in our cities. A massive project, again, with the scale that can get an economic recovery underway post-COVID.
Reverse migration is also an opportunity to collaborate in spreading the geography of development. We have long had policies aimed at getting firms to invest in less-developed districts and the current government has an ambitious goal of doubling farmer’s incomes. But the gap between the richest (urban) and poorest (rural) districts in the country still keeps growing. We need a three-pronged approach: First, as Ashok Gulati has often argued, the easiest way to grow farmer incomes is by having them grow more value-added crops. Fruits and vegetables have great export potential, and exports must be consistently encouraged and not switched on and off as domestic prices change. And the cultivation of palm plantations has the potential for huge import substitution, but, as Gulati points out, we need corporate farming as the gestation period of seven years for the first crop is too much for the average farmer to handle. The Atmanirbhar agricultural reforms, which permit contract farming, and open up agricultural markets, are major medium-term reforms. Implemented right, they can transform agricultural markets. Second, we need to encourage agro-processing near the source. Fostering entrepreneurship in rural and semi-urban areas would combine nicely with local processing. And third, we need to invest even more massively in rural connectivity. Many years ago, the great sociologist Alex Inkeles was asked if there was only one thing that could be done to foster development, what would it be. His answer was to build roads which connect producers to markets, heads to knowledge, and people to each other. Today, we would add digital connectivity to road connectivity to level the playing field for all regardless of where they live.
This must be our programme of work: To fundamentally reform our labour markets, to attract people to our cities where we ensure healthy living conditions, and to create economic opportunities in rural India. The task is huge, and only collaboration between all levels of government (Union, state, and city) and our dynamic private sector can hope to make substantial progress. Let’s use our unprecedented health and economic crisis to truly build a new social contract as our commitment to India@75.
The marriage age misconception
Addressing poverty is the key to improving the health and nutritional status of mothers and their infants
Mary E. John is at the Centre for Women’s Development Studies.

From the ramparts of the Red Fort on Independence Day, the Prime Minister declared that the government is considering raising the legal age of marriage for girls, which is currently 18 years. He said, “We have formed a committee to ensure that daughters are no longer suffering from malnutrition and they are married off at the right age. As soon as the report is submitted, appropriate decisions will be taken about the age of marriage of daughters.” The Committee in question is the task force set up on June 4, announced earlier by the Finance Minister in her Budget Speech. It is widely understood (but not officially stated) that the task force is meant to produce a rationale for raising the minimum age of marriage for women to 21, thus bringing it on a par with that for men.
Population control
Since there is no obvious constituency that has been demanding such a change, the government seems to be motivated by the belief that simply raising the age of marriage is the best way to improve the health and nutritional status of mothers and their infants. Because it flies in the face of the available evidence, we need to ask where this belief is coming from.
One plausible source could be those who advocate for population control and who are influential and whose research is well-funded. Consider, for example, an article published in the prestigious journal The Lancet Child and Adolescent Health, by Nyugen, Scott, Neupane, Tran and Menon, on May 15, 2019. It was funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. This article analyses data on stunting in children and thinness in mothers (as measures of under-nourishment) in the latest round of the National Family Health Survey 4 (2015-16). The paper uses rigorous methods to chase a flawed hypothesis. The authors examine the strength of the association between many different causal factors (the mother’s age at childbearing, her educational level, living conditions, health conditions, decision-making power, and so on) and the health status of mother and child. As it turns out, the poverty of the mother plays the greatest role of all by far — both in relation to her undernourishment and that of her child, but this is not acknowledged. The authors only concede that their cross-sectional design (using data from a single time period) “reduces causal inference. For example, becoming pregnant early might lead to reduced education or wealth; however, a woman from a poor background and lower education might be more likely to become pregnant early.” In other words, instead of early pregnancy causing malnourishment, they may both be the consequences of poverty.
The stated concern of the study was to find ways to break the “intergenerational cycle of undernutrition”. Surely the best way to go about breaking such a cycle would be to pick the factors that are playing the strongest role in perpetuating it. In this case, it would be to address the poverty of the mother, which could be done in a myriad ways, beginning with the most direct method of nutritional programmes for girls and women through a range of institutional mechanisms from Anganwadis to schools. However, the authors choose to concentrate on delaying the age of pregnancy, even though this is the weakest link of all. In fact, age only begins to have some real significance when pregnancies are delayed to ages of 25 and above, which is true of only a minuscule proportion of women in India. The article is unusually generous in its use of the usual scholarly caveats, but leaves itself open to being co-opted by larger agendas driven by the doctrine that “over-population” is the root of all evil in poor countries.
Declining fertility rates
It is unfortunate that such thinking is finding a home in the highest office of the Indian government. Just a year ago, from the ramparts of the same fort, the Prime Minister bluntly declared that “population explosion” was one of India’s major problems. As he put it, “with an ever increasing population, we have to think, can we do justice to the aspirations of our children? Before a child is born in our home, we must ask if we have prepared ourselves to fulfil the child’s needs, or are we going to leave the child to its fate?” Perhaps he (or his advisers) were influenced by the many international reports making alarming predictions about future dystopias that would result if child marriage were not swiftly eliminated in countries like India, which is home to the largest number of underage marriages in the world. It is a pity that those who have the Prime Minister’s ear did not bother to seek the advice of our own demographers who have been studying the apparent link between early marriage and escalating fertility rates for decades. As it turns out, India’s fertility rates have been declining to well below replacement levels in many States, including those with higher levels of child marriage. This could be the reason why those advocating population control have chosen to shift from fuelling fears about booming populations to expressing concern for the undernourishment of children.
Costless and effortless
Perhaps there is a more cynical reason at work. Raising the age at marriage by amending the law is costless and can be effortlessly achieved by legal fiat. Why not claim that doing so will enhance the welfare of women and children, since addressing the true causes of the poor health and nutrition of mothers and children is too difficult a task? The government will not incur any financial costs for raising the age of marriage of girls from 18 to 21 years. But the change will leave the vast majority of Indian women who marry before they are 21 without the legal protections that the institution of marriage otherwise provides, and make their families criminalisable. Those who fervently believe that the minimum age of men and women should be the same in the name of gender equality can suggest that India follow global norms of 18 years for both.
Given the present climate, it could even be that this move is partly prompted by a vague belief that child marriage is more prevalent among Muslims and helps them reproduce faster. The evidence shows that this is not true, but such prejudices are inoculated against all evidence. In this context, it is interesting that the States with high mean ages at marriage of 25 years are erstwhile Jammu and Kashmir, Mizoram, Nagaland, Manipur and Goa. Even Kerala (22 years) and Delhi (23 years) have significantly lower mean ages at marriage.
The proverbial “thinking Indian” — fast becoming an endangered species — has now become accustomed to watching helplessly as acts of state folly unfold. She can also continue to hope for miracles.
सफाई की सीख
संपादकीय
इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने वाले शहरों के शासकों और प्रशासकों के साथ वहां के नागरिक भी प्रशंसा के पात्र हैं। स्वच्छता अभियान को सफलता तभी मिलती है जब सभी मिलकर अपने शहर को साफ-सुथरा बनाने में योगदान देते हैं। इसका बढि़या उदाहरण है इंदौर।इंदौर ने 2017 में देश के सबसे साफ-सुथरे शहर का दर्जा हासिल किया था। तबसे वह लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। इसका मतलब है कि अगर सफाई की बेहतर कार्ययोजना पर अमल करने की इच्छाशक्ति का परिचय दिया जाए और लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए तो उदाहरण पेश किए जा सकते हैं। मुश्किल यह है कि ऐसे उदाहरण अनुकरणीय नहीं बन रहे हैं। इसी कारण यह देखने को मिल रहा है कि जो शहर स्वच्छ सर्वेक्षण की सूची में शीर्ष पर हैं उनके पड़ोसी और कुछ मामलों में तो उनसे सटे शहर कहीं अधिक पीछे दिख रहे हैं। बतौर उदाहरण नई दिल्ली ने स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर स्थान हासिल किया, लेकिन पड़ोसी शहर उसके आसपास भी नहीं दिखे। आखिर सफाई के मामले में जैसा काम नई दिल्ली ने किया वैसा दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी दिल्ली क्यों नहीं कर सकीं? यही बात नवीं मुंबई से सटे इलाकों पर लागू होती है। यदि नवीं मुंबई खुद को साफ-सुथरा रखने की इच्छाशक्ति दिखा सकती है तो उससे सटे शहर क्यों नहीं? आखिर पूरी दिल्ली और पूरी मुंबई बेहतर साफ-सफाई का उदाहरण कब पेश करेंगी? क्या कारण है कि स्वच्छता के मामले में प्रतिस्पद्र्धा का भाव जोर नहीं पकड़ा रहा है?
हालांकि स्वच्छ सर्वेक्षण में कम और अधिक आबादी वाले शहरों का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन इसके आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि ज्यादा आबादी वाले शहरों को साफ रखना कठिन काम है। आबादी से अधिक महत्वपूर्ण है स्वच्छता को लेकर दिखाई जाने वाली संकल्पशक्ति। नि:संदेह साफ-सफाई के मामले में संसाधनों की एक बड़ी भूमिका है, लेकिन वे तभी कारगर साबित हो सकते हैं जब इस इरादे का परिचय दिया जाएगा कि हमें अपने शहर को स्वच्छ बनाना है। यह परिचय केवल इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि स्वच्छता सेहत के साथ पर्यावरण की भी रक्षा करती है, बल्कि इसलिए भी कि उससे देश की छवि निखरती है। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि नगर निकायों को और अधिक जवाबदेह बनाया जाए तथा कचरा निस्तारण के ठोस प्रबंध किए जाएं। स्वच्छता की संस्कृति विकसित करने के लिए यह भी जरूरी है कि घर-परिवार के साथ स्कूलों में साफ-सफाई के महत्व पर और जोर दिया जाए। घर के साथ पास-पड़ोस को भी साफ रखना हमारी आदत बनना चाहिए।
Date:21-08-20
विपरीत धाराओं में फंसी पाकिस्तानी नैया
कश्मीर पर ओआइसी का साथ न मिलने और यूएई के इजरायल से दोस्ती करने के फैसले के बाद पाकिस्तान और गहरे संकट से घिर रहा है।
विवेक काटजू , (लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)
बीते साल पांच अगस्त को भारत ने जम्मू-कश्मीर में जो संवैधानिक बदलाव किए उनके विरोध में पाकिस्तान की हर एक तिकड़म नाकाम रही। इस नाकामी ने पाकिस्तान के राजनीतिक और सामरिक वर्ग को कुंठित कर दिया है। यह कुंठा दूसरे देशों के रवैये को लेकर पाकिस्तानी मंत्रियों के बयानों से साफ जाहिर भी हो रही। अब तो कश्मीर के मसले पर भी पाकिस्तानी मंत्रियों के मतभेद सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान अरब में अपने सबसे बड़े रहनुमा सऊदी अरब पर परोक्ष रूप से आरोप लगा चुका है। वहीं एक पाकिस्तानी कैबिनेट मंत्री ने अपने ही विदेश मंत्री को आड़े हाथों लिया कि वह कश्मीर के मसले को ढंग से संभाल नहीं पाए। यह तो उस सिद्धांत के ही खिलाफ है जिसके तहत सरकारें काम करती हैं। पाकिस्तान के एक और अरबी रहनुमा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी हाल में इजरायल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित करके उसकी मुश्किलें और बढ़ा दीं। ऐसा करने वाला यूएई अरब का तीसरा देश है। इससे पहले 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन भी ऐसा कर चुके हैं। यूएई का फैसला पाकिस्तान को बड़ी दुविधा में डाल रहा है, क्योंकि इसने अरब और मुस्लिम देशों के बीच विवाद पैदा कर दिया है जिसमें पाकिस्तान को पता नहीं कि किसका समर्थन करना है?
पाकिस्तान ने पांच अगस्त का दिन यौम-ए-इस्तेहाल यानी कश्मीर घेराबंदी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान साल भर पहले भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर में उठाए गए कदम की कड़ी निंदा की गई। तुर्की को छोड़कर किसी भी प्रमुख मुस्लिम देश ने पाकिस्तानी दुष्प्रचार पर कान नहीं दिया। दुनिया की किसी बड़ी शक्ति ने भी कोई टिप्पणी नहीं की। केवल चीन ही अपवाद रहा, लेकिन उसका भारत विरोधी रुख किसी से छिपा नहीं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने वैश्विक मतभिन्नता पर खासी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्हें यह महसूस होना चाहिए था कि दुनिया ने इसे भारत के आंतरिक मामले के रूप में ही देखा। कुरैशी ने इस्लामिक देशों के संगठन यानी ओआइसी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि ओआइसी ने कश्मीर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। दरअसल पाकिस्तान कश्मीर पर ओआइसी के विदेश मंत्रियों की एक बैठक आयोजित कराना चाहता था। चूंकि सऊदी अरब ओआइसी का मुख्य कर्ताधर्ता है इसलिए यह उसकी ही आलोचना मानी गई। कुरैशी ने यहां तक कह दिया कि यदि ओआइसी कुछ नहीं करता तो वह इमरान खान को सलाह देंगे कि वह ऐसे इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित करें जो कश्मीर पर बैठक के इच्छुक हों।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विदेशी मदद पर निर्भर है और सऊदी अरब उसके सबसे बड़े मददगार देशों में से एक है। वह उसे लंबी उधारी पर तेल देता है। पाकिस्तानी आलोचना से कुपित सऊदी अरब ने पाक से उसके एक अरब डॉलर लौटाने के लिए कहा। इसने पाकिस्तानी सरकार और सेना, दोनों को तगड़ा झटका दिया। यह साफ था कि कुरैशी की बयानबाजी से सेना भी खुश नहीं थी। उसने मानवाधिकार मंत्री शिरीन माजरी को संकेत किया कि वह विदेश मंत्री की आलोचना करें। इसके बाद माजरी ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीरियों के लिए जो किया उसे आगे बढ़ाने में विदेश मंत्रालय पूरी तरह नाकाम रहा। उनके मुताबिक सोशल मीडिया के दौर में विदेश मंत्री परंपरागत कूटनीति का दामन पकड़े रहे। केवल भाषणबाजी में लगे रहे। माजरी कट्टर भारत विरोधी रही हैं और भारत पर उनका रुख पाकिस्तानी फौज के अनुरूप ही रहा है।
कश्मीर के मसले पर अन्य देशों को अपने पाले में लाने में पाकिस्तान की नाकामी के लिए उसकी कूटनीति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि असल कारण यह है कि दुनिया उसे आतंक की धुरी और कश्मीर में दखलंदाजी करने वाला मानती है। इन बुनियादी पहलुओं को दुरुस्त किए बिना पाकिस्तानी नेता एक-दूसरे से भिड़ रहे हैं। यह स्थिति इमरान सरकार को शर्मसार करने वाली है। देखना होगा कि इमरान अपनी कैबिनेट में इतने गहरे मतभेदों से कैसे निपटते हैं? सऊदी अरब का गुस्सा शांत करने के लिए सेना प्रमुख कमर बाजवा को वहां जाना पड़ा। अगर सऊदी अरब ने कुरैशी को हटाए जाने की मांग रखी तो इमरान के पास ऐसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा उसके गुलाम की तरह काम करता आया है। कई बार तो घरेलू राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने के लिए भी सऊदी अरब की मदद ली जाती रही है।
इस बीच यूएई द्वारा इजरायल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध बनाने से भी पाकिस्तान और मुश्किल में पड़ा है। सऊदी अरब ने अभी तक इस मसले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वह इससे नाखुश भी नहीं है। दूसरी ओर तुर्की और ईरान ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस तरह इस्लामिक जगत के बीच मौजूदा खाई और गहरी हो गई है। इसने पाकिस्तान को भारी दुविधा में धकेल दिया है। वह खुद को एक प्रमुख मुस्लिम शक्ति के रूप में पेश करता आया है, क्योंकि वही इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि अपने तंगहाल र्आिथक हालात और आतंक को पालने-पोसने की वजह से इस्लाम को बदनाम करने के कारण उसे मुस्लिम जगत में कोई सम्मान नहीं मिला।
पिछले साल दिसंबर में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी जब सऊदी अरब के दबाव में उसे कुआलालंपुर में तुर्की और मलेशिया द्वारा आयोजित सम्मेलन में शिरकत करने का इरादा छोड़ना पड़ा था। सऊदी को यह बर्दाश्त नहीं कि कोई उसके नेतृत्व को चुनौती दे। उसे लगा कि तुर्की के साथ गलबहियां कर इमरान विरोधी पाले में जा रहे हैं। इसके अलावा सऊदी और ईरान के बीच प्रतिद्वंद्विता का पहलू भी है जिसके राजनीतिक एवं धार्मिक दोनों निहितार्थ हैं। अतीत में दोनों देश पाकिस्तान के सुन्नी और शिया समूहों को शह देते आए हैं जिनमें भारी हिंसक टकराव हुए हैं। अब जब यूएई ने फलस्तीन के मसले को लगभग त्याग दिया है तो यह पाकिस्तानी धरती पर नए सिरे से मजहबी हिंसा भड़कने का कारण बन सकता है। देखना है कि पाकिस्तान इन विपरीत धाराओं में अपनी नैया को कैसे पार लगाता है? कश्मीर को लेकर उन्माद दिखाने के कारण उसकी विदेश नीति के लिए संकट और बढ़ता जा रहा है।
![]() Date:21-08-20
Date:21-08-20
घर से काम का चलन लाएगा बड़े परिवर्तन!
अजित बालकृष्णन , (लेखक इंटरनेट उद्यमी एवं आईआईएम कलकत्ता के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पूर्व चेयरमैन हैं)
‘अजित, तुम इतने व्यस्त क्यों रहते हो? तुम अपना काम दूसरों के सुपुर्द करना क्यों नहीं सीखते? इससे तुम पर्यवेक्षण का काम अच्छी तरह कर पाओगे।’ मुझे ऐसी दोस्ताना सलाह मेरे कामकाजी सहयोगी पहले दिन से ही देते रहे हैं। मुझे लगता है कि 1970 के दशक में भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) कलकत्ता से निकलने के बाद मैं शुरुआती कामकाजी दिनों में खासा समय फेसिट कैलकुलेटिंग मशीन पर बिताया करता था। बाद में उस मशीन की जगह पर्सनल कंप्यूटर ने ले ली। जब भी मुझे ऐसी सलाह मिलती है तो मैं मुस्कराते हुए कहता हूं, ‘मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा ताल्लुक ऐसे किसान खानदान से है जो अपने हाथों से खेत की जुताई करने एवं घास काटने के आदी हैं।’ फिर मुझे सलाह देने वाला शख्स यह सोचने लगता है कि मैंने कोई जातिवादी टिप्पणी तो नहीं कर दी है। लेकिन ऐसी बातें करने और मजाक करने का मेरा कोई इतिहास न होने से वह चला जाता है।
किसी भी प्रबंध जर्नल पर सरसरी नजर भी डालें तो आपको प्रत्यायोजन के बारे में पढऩे को जरूर मिल जाएगा। अब प्रबंधन की बाइबिल कही जाने वाली हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू को ही लें, उसमें आपको महान नेता बनने के लिए यह सीखना जरूरी बताया गया है कि प्रत्यायोजन बेहतर ढंग से कैसे करें? इस बारे में सुझावों की भरमार है कि प्रत्यायोजन किस तरह और क्यों करें? हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू पत्रिका की ही सलाह है, ‘ऐसे तमाम कारण हैं जिनकी वजह से प्रबंधक अपना दायित्व दूसरों को नहीं सौंपते हैं। कुछ पूर्णतावादी होते हैं जिन्हें लगता है कि हर काम खुद कर लेना कहीं आसान है या फिर वे अपने काम को दूसरों से बेहतर मानते हैं।’ एक प्रबंधक को लगातार ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया जाता है जो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह बोलता है लेकिन किसी जटिल गुणा-भाग या किसी संभावित ग्राहक को सामान बेचने में अपना सिर नहीं खपाता है। इसी तरह किसी मीडिया कंपनी के प्रबंधक से साक्षात्कार लेने और लेख लिखने की अपेक्षा नहीं की जाती है। प्रबंधक से दूसरों के काम में समन्वय बिठाने के लिए महंगे सम्मेलन कक्ष में बैठक लेने की उम्मीद होती है। मेरी दृढ़ धारणा है कि जमीनी काम से दूर रहने वाले ऐसे प्रबंधकों की दुनिया अचानक ही ढहने वाली है। ऐसा कोविड-19 महामारी के प्रसार और उसकी वजह से कर्मचारियों के बीच घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) की नई प्रवृत्ति के कारण हो सकता है। संचार एवं शेयरिंग करने वाले सॉफ्टवेयर टूल्स की अचानक भरमार होने से समन्वय एवं बंदोबस्त करने का वह काम काफी हद तक हो जा रहा है जो परंपरागत तौर पर इन प्रबंधकों का दायित्व माना जाता रहा है।
दुनिया भर में कंपनियां बड़ी शिद्दत से यह पता लगाने की कोशिश में जुटी हैं कि किस तरह के कामों को वर्क फ्रॉम होम की श्रेणी में रखा जाए और किस तरह के काम वर्क फ्रॉम ऑफिस श्रेणी में गिने जाएं। क्या यह विभाजन इस आधार पर होना चाहिए कि वह काम उस कंपनी के लिए कितना अहम है? इस तरह से निर्धारण करने पर उतने अहम नहीं माने जाने वाले कार्यों को वर्क फ्रॉम होम श्रेणी में डाला जा सकता है। क्या आने वाले समय में कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में इस आधार पर भी विभेद देखने को मिलेगा कि अमुक काम किस श्रेणी में आता है? क्या वर्क फ्रॉम होम श्रेणी वाले कार्यों को आउटसोर्स कर किसी छोटे ठेकेदार को दे दिए जाएगा?
ऐसी निराशाजनक भविष्यवाणियों के बीच थोड़ा ठहरकर सांस लेना सही होगा। ऐसी स्थिति में इतिहास पर नजर डालने से कुछ सबक सीखे जा सकते हैं।
पहली बात तो यह है कि कर्मचारियों को कारखाने और फिर दफ्तर में एक साथ इकट्ठा करना कोई प्राचीन अवधारणा नहीं है। लोगों के एक समूह के एक छत के नीचे काम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें सीधी निगरानी में रखने की अवधारणा 18वीं सदी के आखिर में इंगलैंड में हुई प्रथम औद्योगिक क्रांति की ही देन है। सूत कातने वाली बड़ी मशीन वाटरफ्रेम के आविष्कारक रिचर्ड आर्कराइट को जल्द ही अहसास हो गया कि उनकी मशीन इतनी बड़ी है कि किसी एक घर में उसे नहीं रखा जा सकता है। फिर आर्कराइट ने इस मशीन को इंगलैंड के डर्बीशर स्थित एक बड़ी जगह पर लगाया और सभी श्रमिकों को क्रॉमफोर्ड मिल नाम की फैक्टरी में इकट्ठा बुलाया। उसके पहले तक पूरी दुनिया में धागे की कताई एवं कपड़े की बुनाई का सारा काम कारीगर अपने घरों में रहकर यानी वर्क फ्रॉम होम करते आए थे।
आर्कराइट की वाटरफ्रेम मशीन के आविष्कार ने फैक्टरी की अवधारणा को जन्म देने के साथ इसका विस्तार भी किया। इसी के साथ बैंकिंग, रेल, बीमा एवं टेलीग्राफी जैसे उद्योगों के समानांतर विकास ने भी क्लर्कों की जरूरत पैदा की। मिले हुए ऑर्डर को पूरा करने, अकाउंटिंग और कागजात को व्यवस्थित रखने की जरूरत पूरी करने के लिए क्लर्कों की दरकार थी। इन सभी चीजों के एक साथ इकट्ठा होने पर ऑफिस यानी दफ्तर का स्वरूप सामने आया। माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन की लीडेनहॉल स्ट्रीट में 1729 में खुला कार्यालय दुनिया का पहला बड़ा ऑफिस था। इस दफ्तर से कंपनी के अफसर उपनिवेशों में कारोबार का संचालन करते थे।
शुरुआती दिनों से ही दफ्तरों एवं कारखानों की प्रगति इतनी तीव्र रही है कि वह आधुनिकता एवं प्रगति के प्रतीक बनते गए और घर में रहते हुए काम करने की पुरानी परिपाटी को पिछड़े एवं गंवार लोगों का काम माना जाने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले हरेक मध्यवर्गीय बच्चे की चाहत ‘ऑफिस जॉब’ पाने की हो गई। आखिर दफ्तरों में किए जाने वाले काम को आधुनिक माना जाता था।
बहुत जल्द बिज़नेस स्कूल भी नमूदार हो गए। इनकी शुरुआत अमेरिका में हुई और फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी वे नजर आने लगे। ये बिज़नेस स्कूल दफ्तर में काम करने के सही एवं गलत तरीकों के बारे में उपदेश देने लगे। समाजशास्त्रियों एवं मनोविज्ञानियों ने आपसी गठजोड़ कर सांगठनिक व्यवहार के बारे में कई सिद्धांत पेश किए, संगठन के भीतर कर्मचारियों की भूमिका एवं संबंधों और दायित्वों को परिभाषित भी किया गया। ये सारे सिद्धांत वर्क फ्रॉम ऑफिस संगठन के लिए प्रतिपादित किए गए थे। यहां तक कि प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के लिए पोशाकें भी निर्धारित की गईं। ऑफिस जॉब और इसकी संस्कृति सामंती ढांचे खासकर भारत में बखूबी फिट बैठी। इस तरह एक प्रबंधकीय तबका सामने आया जो बंद केबिन में बैठता था और लंबी कतारों में लगी मेजों पर तैनात कमतर लोगों के काम की निगरानी करने के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठक करने में व्यस्त रहता था।
दुनिया के कई प्रतिष्ठित संगठन इस समय अपने 60-70 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम ढांचे में ही बनाए रखने के बारे में सोच रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था की तरफ अचानक हुए इस बड़े झुकाव से मध्यवर्ग की उस जानी-पहचानी दिनचर्या में कहीं नाटकीय बदलाव तो नहीं आने वाला है। आखिर अभी तक एक मध्यवर्गीय व्यक्ति सुबह जगने के बाद नहा-धोकर तैयार होने, नाश्ता करने, काम पर जाने, दिन भर दफ्तर में बिताने और शाम को वापस घर लौटने की दिनचर्या का कितना अभ्यस्त हो चुका है।
क्या आईआईएम समेत तमाम प्रबंध शिक्षण संस्थानों को जल्द ही अपने पाठ्यक्रम में बदलाव कर अपने छात्रों को यह बात भी सिखानी पड़ेगी कि उन्हें भी पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई संस्थानों से निकले युवाओं की तरह अपने हाथों से ही काम करने होंगे ?
सुविधा की भर्ती
संपादकीय
सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर युवाओं को साल भर परेशान होते देखा जाता है। अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से रिक्तयां विज्ञापित और फिर उनके लिए चयन प्रक्रिया शुरू करते देखे जाते हैं। ऐसे में युवाओं को हर विभाग और हर रिक्ति के लिए अलग-अलग आवेदन करने और फिर उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। इस तरह उनका समय और पैसा दोनों काफी बर्बाद होता है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी गैर-तकनीकी पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के मकसद से राष्ट्रीय भर्ती एजंसी गठित करने का फैसला किया है। अभी तक रेलवे, बैंकिंग जैसे विभिन्न सरकारी विभागों की भर्तियों के लिए करीब बीस आयोग काम करते हैं। अब उन्हें राष्ट्रीय भर्ती एजंसी में समाहित कर दिया जाएगा। अगले तीन सालों में यह एजंसी पूरी तरह काम करने लगेगी। इसके तहत सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को इधर-उधर न भटकना पड़े। जाहिर है, इस एजंसी के गठन से युवाओं को नौकरियों के लिए आवेदन करने से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने तक में काफी सहूलियत होगी।
केंद्रीय और राज्य स्तर की प्रशासनिक सेवाओं के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन संघ लोकसेवा आयोग और राज्यों के आयोग करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से नीचे के पदों, जैसे सचिवालयों आदि के कर्मियों की भर्तियां कर्मचारी चयन आयोग करता है। पर रेलवे, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में भर्ती के अपने बोर्ड हैं। अब प्रशासनिक पदों को छोड़ कर सभी विभागों की भर्ती प्रक्रिया एक ही केंद्रीकृत एजंसी कर सकेगी। इस तरह बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड और कर्मचारी चयन आयोग एक में समाहित हो जाएंगे। जाहिर है, इससे न सिर्फ युवाओं की परेशानी कम होगी, बल्कि विभिन्न विभागों का खर्च भी बचेगा। लोकसेवा आयोग और राज्यों के आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं का समय लगभग तय है। इसी तरह कर्मचारी चयन आयोग की रिक्तियों और परीक्षाओं का समय भी निश्चित है, इसलिए युवा उनके लिए पहले से तैयार रहते हैं। फिर उनमें अनेक पदों के लिए एक ही आवेदन करना पड़ता है, एक ही बार शुल्क जमा करना होता है, इसलिए अलग-अलग फीस भरने और बार-बार परीक्षा की तैयारी करने की झंझट नहीं रहती। जिन विभागों की भर्तियों के लिए अलग से प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उनका समय भी तय नहीं होता और वे अपने तरीके से पर्चे तैयार करते हैं, इस तरह अलग-अलग विभागों के अलग-अलग परीक्षा प्रारूप हैं। स्वाभाविक ही, इस तरह युवाओं को हर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी पड़ती है। लिहाजा, उन पर साल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करने का दबाव और तनाव बना रहता है।
पहले इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए भी इसी तरह युवाओं को अलग-अलग आवेदन करने और भाग-दौड़ कर परीक्षाएं देनी पड़ती थीं। उन्हें केंद्रीकृत किया गया और फिर उनके लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी का गठन किया गया। इससे उन परीक्षाओं में विद्यार्थियों को काफी सहूलियत हो गई। उसी तरह नई गठित राष्ट्रीय भर्ती एजंसी भी काम करेगी और युवाओं, अभिभावकों, विभिन्न विभागों सभी के लिए सहूलियत हो जाएगी। अभी तक केंद्रीकृत व्यवस्था न होने की वजह से युवाओं, खासकर लड़कियों के साथ उनके अभिभावकों को भी विभिन्न परीक्षा केंद्रों के चक्कर काटने पड़ते थे। विकलांग लड़कियों के लिए अलग तरह की परेशानियां उठानी पड़ती थीं। अब उन सारी झंझटों से मुक्ति का रास्ता खुलेगा।
