
20-02-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
क्या ऐसी नीतियों से देश में रोजगार बढ़ पाएगा?
संपादकीय
अध्ययनों में पता चला है कि पिछले कई वर्षों से निजी उद्यमों और कॉर्पोरेट घरानों की आय व संपत्ति तो बेतहाशा बढ़ी है, लेकिन उसकी तुलना में मजदूरों या वेतनभोगियों की पगार कम हुई है। जाहिर है आयकर और अन्य करों में छूट का मूल आशय है उद्यम को बढ़ावा देना, ताकि व्यापार और रोजगार बढ़े। लेकिन राज्यसभा में सरकार की रिपोर्ट से पता चला कि छूट का लाभ तो उद्यमियों ने खूब लिया, लेकिन उद्यम में विकास की जगह इस पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट बनाने में किया। सरकार से सवाल पूछा गया था कि इन छूटों के बाद उद्योगों ने कितनी ज्यादा नौकरियां दीं। सरकार का जवाब था- ‘नहीं मालूम’। हालांकि सरकार को ईपीएफ, ईएसआईसी और श्रम विभाग से यह आंकड़ा आसानी से मिल सकता था। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखें। सरकारी व्यय में सबसे प्रमुख होता है पूंजीगत निवेश । इस मद में खर्च होने वाला हर एक रुपया करीब 2.50 रुपए देश की अर्थव्यवस्था में जोड़ता है। लेकिन जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत में चीन, ब्राजील और फ्रांस जैसे देशों से काफी कम खर्च इस मद में होता है। अगर उद्योगपति फैक्ट्री बनाने की जगह जमीन खरीदने में पैसा लगा रहे हैं तो फिर उन्हें क्यों छूटें दी जाएं? अगर अमेरिका अपने ‘किंग साइज’ प्रशासनिक ढांचे को उत्पादक बनाने की कोशिश कर रहा है तो भारत को भी दो करोड़ कर्मचारियों-अफसरों वाले सरकारी ढांचे की उपादेयता देखनी होगी।
Date: 20-02-25
अब भारत लौटकर आ रही हैं पेशेवर प्रतिभाएं
मिन्हाज मर्चेंट, ( लेखक, प्रकाशक और सम्पादक )
भारत के आलोचक आरोप लगाते हैं कि हमारे पेशेवर विदेश जा रहे हैं, क्योंकि देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। उनका कहना है कि पश्चिम की ओर पलायन करने वाले प्रतिभावान लोगों में भारत के बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर और उद्यमी शामिल हैं। जबकि सच यह है कि प्रतिभा एक परिवर्तनशील वस्तु है। यह दोनों ओर बहती है। कई भारतीय उद्यमी और पेशेवर- जो एक दशक पहले भारत छोड़ गए थे- वे आज भारत लौट भी रहे हैं। इसके खासे कारण हैं कि क्यों ऐतिहासिक ‘ब्रेन-ड्रेन’ (प्रतिभा-पलायन) भारत के लिए ‘ब्रेन-गेन’ (प्रतिभाओं की प्राप्ति) में परिवर्तित होने लगा है।
सिलिकॉन वैली के अग्रणी उद्यमी विवेक वाधवा का उदाहरण लीजिए। हाल ही में प्रकाशित एक लेख में वाधवा ने बताया कि क्यों प्रतिभाशाली भारतीय अमेरिका में सफल करियर बनाने के बाद भारत में अपने विश्वास और पैसों का निवेश कर रहे हैं। वे लिखते हैं कि अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियों से तंग आकर उच्च-कुशल भारतीय पेशेवर बड़ी संख्या में घर लौटकर आ रहे हैं और अपने साथ बेशकीमती विशेषज्ञता, बेहतरीन नेटवर्क और अच्छी-खासी धनराशि लेकर लौट रहे हैं। यह ‘रिवर्स ब्रेन-ड्रेन’ भारत की इनोवेशन-इकोनॉमी को पोषित कर रहा है।
वाधवा आगे बताते हैं कि वायोनिक्स बायोसाइंसेस के साथ उनका अनुभव इस बिंदु को और स्पष्ट करता है। उन्हें विदेश से प्रतिभाओं को नियुक्त करना पड़ता था और जटिल वीजा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। इमिग्रेशन-विरोधी भावनाओं और नौकरशाही की लेटलतीफी के कारण समय पर अच्छी टीम बनाना लगभग बहुत कठिन हो जाता था। इन चुनौतियों के चलते उन्होंने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) ऑपरेशंस को भारत में स्थानांतरित कर दिया, जहां उच्च-कुशल टैलेंट पूल तक आसान पहुंच थी, अनावश्यक लालफीताशाही नहीं थी और इनोवेशन को गति दी जा सकती थी।
अन्य उद्यमियों का कहना है बात केवल लागतों की ही नहीं। आज भारत का तकनीकी स्किलसेट भी विश्वस्तरीय हो गया है। यही कारण है कि 1,600 से अधिक बड़ी विदेशी कंपनियों ने भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) स्थापित किए हैं। ये केंद्र जटिल इंजीनियरिंग, आरएंडडी तथा अत्याधुनिक तकनीकी इनोवेशन करते हैं। उन्होंने सर्वोत्तम स्थानीय प्रतिभाओं की भर्ती के लिए टीसीएस और इंफोसिस जैसी भारतीय सूचना-प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है।
हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। भारत विविधताओं से भरा देश है। उसका एक हिस्सा पहले से ही विकसित राष्ट्र है। दूसरा हिस्सा तेजी से विकसित हो रहा है। तीसरे को विकसित होने में समय लगेगा। विकसित भारत का लक्ष्य रखते समय योजनाकारों को समझना होगा कि भारत अलग-अलग समय पर विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करेगा, जिसे मोटे तौर पर प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक और अन्य मापदंडों पर परिभाषित किया जाता है।
भारत में जर्मनी के पूर्व राजदूत वाल्टर जे. लिंडनर ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि भारत को विकासशील या विकसित के रूप में वर्गीकृत करना कठिन है। बेंगलुरू, पुणे और हैदराबाद जैसे शहर विकसित लगते हैं, जबकि भारत के गांव-देहात आज भी सदियों पीछे मालूम होते हैं। यह द्वंद्व ही भारत को जटिल और आकर्षक बनाता है। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण अब प्रायः उपयुक्त नहीं रह गए हैं। ‘विकसित’ का मतलब क्या है, यह कौन तय करता है? इनमें से कई परिभाषाएं पश्चिमी संस्थाओं से आती हैं।
विदेशों में रहकर काम करने वाले भारतीय इसे समझते हैं। जब देश की समाजवादी आर्थिक नीतियों ने यहां जीवन कठिन बना दिया था तो कई लोगों ने भारत छोड़ दिया। तब पश्चिम ने उनसे बेहतर भविष्य का वादा किया था। लेकिन आज वैसी बात नहीं है, क्योंकि अनेक पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना कर रही हैं। ट्रम्प की इमिग्रेशन विरोधी नीतियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमिका चाहने वाले तकनीकी विशेषज्ञों और पेशेवरों के बीच ‘रिवर्स ब्रेन-ड्रेन’ में तेजी देखी जा सकती है। भारतीय प्रवासियों के प्रति अमेरिका की नस्लवादी घृणा कोई नई बात नहीं है। जैसा कि राजमोहन गांधी ने हाल ही में एक लेख में बताया कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 1923 में एक निर्णय सुनाया था कि ‘भारतीय नागरिकता के लिए अयोग्य हैं!’
1960 के दशक के मध्य में जाकर भारतीयों को यूएस वर्क-वीजा दिया जाने लगा। इसके परिणामस्वरूप वहां जाने वाले भारतीय पेशेवरों की संख्या में वृद्धि हुई। इसने अगली आधी सदी तक भारत से ब्रेन-ड्रेन को परिभाषित किया। लेकिन अब यह प्रवाह उलट रहा है। जैसा कि वाधवा बताते हैं, चीनी ग्रंथों के विशाल संग्रह पर प्रशिक्षित होने से डीपसीक ने चीन की समृद्ध सांस्कृतिक, दार्शनिक और साहित्यिक विरासत को आत्मसात कर लिया है। यह बताता है कि घरेलू डेटा पर एआई का विकास केवल भाषा के बारे में नहीं है- यह कृत्रिम मेधा की मूल प्रकृति को भी आकार देता है।
इन मायनों में तो भारत एआई के भविष्य को और अधिक पुनर्परिभाषित कर सकता है, क्योंकि हमारे यहां वेद, उपनिषद्, अर्थशास्त्र, संगम-साहित्य की महान परम्परा रही है। इस तरह के अवसर ही भारत को विकसित बनाएंगे, लेकिन यह एक साथ नहीं, बल्कि अंशों में होगा। प्रतिभाओं का भारत लौटकर आना इसी प्रक्रिया में है। अपने देश में काम करने के बेहतर मौके मिल रहे हैं… अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियों से तंग आकर उच्च-कुशल भारतीय पेशेवर बड़ी संख्या में घर लौटकर आ रहे हैं और अपने साथ बेशकीमती विशेषज्ञता, बेहतरीन नेटवर्क और अच्छी-खासी धनराशि लेकर लौट रहे हैं।
Date: 20-02-25
गलत सूचनाओं के इस दौर में चुनौतियां भी काफी बढ़ी हैं
कौशिक बसु, ( विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट )
पूरी दुनिया में ही आज लोकतंत्र चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तानाशाह चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंक रहे हैं और सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। सत्तावादी नेताओं का बढ़ता प्रभाव अब भी सुर्खियां बनाता है, लेकिन वे स्वतंत्र समाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं रह गए हैं। वास्तविक खतरा अधिक घातक है : लोकतांत्रिक प्रणालियों में धीरे-धीरे किन्तु बहुत गहरे बदलाव।
ऊपर से देखने पर सब ठीक लगता है। चुनाव बदस्तूर हो रहे हैं और मतदाता उन नेताओं को चुन रहे हैं, जिनके बारे में उनका मानना है वे उनके हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन अक्सर वे ऐसे राजनेताओं को चुन लेते हैं, जो केवल अपने हितों की रक्षा करते हैं। हालांकि वोटरों का बहकावे में आना कोई नई बात नहीं, लेकिन अब यह इतना व्यापक हो गया है कि लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद के लिए खतरा बन गया है।
दुनिया भर के आम लोग आज जोशो-खरोश से उन नेताओं का समर्थन कर रहे हैं, जिन्हें उनकी परवाह नहीं। लोकसेवा के प्रति इन नेताओं की प्रतिबद्धता शोचनीय है। वे अपने और अपने साथियों (क्रोनीज़) के लिए अधिक से अधिक सम्पदा और सत्ता की खोज में लगे रहते हैं। मुख्यधारा के अर्थशास्त्री और राजनीतिक वैज्ञानिक लंबे समय से ‘मध्यमार्गी मतदाता सिद्धांत’ पर भरोसा करते आ रहे हैं, जिसके मुताबिक बहुमतवादी चुनावी प्रणाली में राजनेता स्वाभाविक रूप से मध्यमार्गी मतदाताओं की प्राथमिकताओं की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उन्हें आकर्षित करना आवश्यक है। लेकिन आज के गहराते राजनीतिक ध्रुवीकरण और नेताओं में कट्टरपंथी रुख अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति से पता चलता है कि यह धारणा अब टिक नहीं पाती।
इस बदलाव का सोशल मीडिया के उदय के साथ गहरा संबंध है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म सूचनाप्रद विमर्श को बढ़ावा देने के बजाय गलत सूचना फैलाने के शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं, जिससे अवसरवादी नेता आसानी से लोगों को गुमराह करने और उन्हें प्रभावित करने में सक्षम हो गए हैं। प्राचीन एथेंस में अपनी स्थापना के बाद से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए हैं। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है, पहले की लोकतांत्रिक प्रणालियों की कुछ विशेषताएं पुरानी होती जाती हैं। नैतिक मानदंडों के विकास से भी मौलिक सुधार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, रोमन गणराज्य में उच्च पदस्थ अधिकारियों और धनी लोगों के वोटों का महत्व आम नागरिकों के वोटों से अधिक हुआ करता था। लेकिन आज हम इसे स्वीकार्य नहीं मानते। इसी तरह जैसे-जैसे लोकतंत्र विकसित हुआ, स्थिरता की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। इसके परिणामस्वरूप ही संविधानों की शुरुआत हुई। यद्यपि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए साधारण बहुमत से अधिक की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुख्य संवैधानिक संस्थाओं में मनचाहे बदलाव न किए जा सकें।
लोकतांत्रिक शासन पर बढ़ते दबाव के कारण दुनिया एक बार फिर अपने को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों और सोशल मीडिया के उदय ने सुपर-रिच लोगों को जनमत को आकार देने के लिए नए साधन उपलब्ध करा दिए हैं। मतदाताओं को लगता है कि वे लोकतंत्र में सक्रिय भागीदार हैं, जबकि वास्तविक सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित है।
इस प्रकार की असमानता पर अंकुश लगाना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है; बल्कि लोकतंत्र को अधिनायकवाद के खतरे से बचाना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, हमें एक ऐसी कर प्रणाली की आवश्यकता है, जो इनोवेशन और उद्यमशीलता को बाधित किए बिना धन और आय का पुनर्वितरण करे।
जब सुपर-रिच लोग समृद्धि के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वे अधिक धन कमाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपने जैसे धनकुबेरों से आगे निकलने की लालसा से प्रेरित होते हैं। इसमें एक ऐसे कर को लागू करने का अवसर है, जिसे मैं ‘अकॉर्डियन टैक्स’ कहता हूं। इसमें उच्च आय वालों पर कर लगाकर उससे प्राप्त राजस्व को कम आय वालों के बीच इस तरह से पुनर्वितरित किया जाता है कि अमीरों के बीच सापेक्ष रैंकिंग बरकरार रहे। लेकिन विषमता का मुकाबला करना अकेले देशों के बूते की बात नहीं, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है।
Date: 20-02-25
मुद्दा रणवीर इलाहाबादिया नहीं, ‘जेन-ज़ी’ होना चाहिए
मुकेश माथुर, ( दैनिक भास्कर )
‘रणवीर इलाहाबादिया पर प्रतिबंध लगा दो। जिस चैनल पर उसने वाहियात बातें बोलीं, उसे बंद कर दो। अश्लीलता फैला रहे सभी चैनल ऑफ-एयर हो जाने चाहिए। ओटीटी का भी कुछ करो। इस लड़के का अपना पॉडकास्ट भी बंद करवा दो।’
मानो राष्ट्र की दशकों से सोई चेतना जाग गई है। रणवीर पर रिपोर्टें दर्ज हो गई हैं। बस, उसका किस्सा खत्म हो जाना चाहिए। समाज को चैन मिले।
हम हर घटना में एक आरोपी ढूंढ़ते हैं और उसे नेस्तनाबूद करने में जुट जाते हैं। सहूलियत का काम। जो मुश्किल काम है वो यह कि उस घटना से एक विमर्श शुरू हो। कारणों में जाएं। बदलावों को पहचानें। वे बदलाव जो ऐसी घटना को जन्म दे रहे हैं। इसके बाद…। समाज-सरकार-तंत्र जुटे। चीजें ठीक करने में। कोर्स करेक्शन में।
इलाहाबादिया को ही लीजिए। उसने जो बोला। निम्न स्तर का। आप कितने ही लिबरल हों, वह जो कह रहा है, उसे सुनकर माथे पर शिकन आएगी ही। क्या हम हजारों साल लगाकर सभ्यता की सीढ़ियां इसलिए चढ़े हैं कि अनाचार-व्यभिचार और स्वच्छंदता के कुएं में कूद जाएं? असंभव।
लेकिन इलाहाबादिया पर देश भर में एफआईआर कराने से ज्यादा जरूरी काम दूसरे हैं। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी लेकिन और गंभीरता लिए। चिंता हो जानी चाहिए थी कि जिस ‘जेन-ज़ी’ को यूट्यूबर समय रैना का यह शो रिप्रजेंट कर रहा है, उस पीढ़ी को हुआ क्या है? क्यों इस पीढ़ी को वर्जनाएं तोड़ना, वर्जित बात कहना-सुनना थ्रिल देता है?
यूं यह हमेशा से ही इंसान को थ्रिल देता आया है, लेकिन कोविड के मुश्किल दिनों में बंद कमरों में बचपन के कीमती साल स्क्रीन के साथ बिताने वाली पीढ़ी उन महीन सीमारेखाओं को ही नहीं पहचानती, जो घर-समाज में आपके बोल-चाल, हाव-भाव, व्यवहार को लेकर बनी हैं।
यह पीढ़ी सारे सुख तो लेना चाहती है लेकिन जीवन में कैजुअल न होने की न्यूनतम जिम्मेदारी कंधे पर लेकर बड़ी नहीं होना चाहती।
1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुए इन लोगों के साथ कई ऐसी चीजें जुड़ी हैं, जो इनसे पहले के मिलेनियल्स और उससे पहले की पीढ़ियों के साथ नहीं थीं। यह पहली पीढ़ी है, जिसे जन्म के बाद से ही इंटरनेट मिला है। हमने स्मार्टफोन के पहले की जिंदगी भी देखी है, बाद की भी।
हमने दुनियादारी दुनिया में जाकर सीखी है, जबकि ‘जेन-ज़ी’ के लिए स्क्रीन ही दुनिया है।
जाहिर है उस तरह का व्यक्तित्व विकास, रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझने का माद्दा पैदा हो ही नहीं पाया। कोचिंगों में बच्चों की आत्महत्या की कोई भी खबर आने पर हम कह देते हैं- माता-पिता का दबाव सबसे बड़ा कारण है। मैं कहता हूं कि नई पीढ़ी के बच्चे ही भीतर से कमजोर हैं, हल्के-से झटके से टूट जाते हैं।
इंटेलिजेंट डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में केवल 25 प्रतिशत कंपनियां ही ‘जेन-ज़ी’ को नौकरी देने को तैयार हैं। 21 प्रतिशत मैनेजर कहते हैं कि इस पीढ़ी के युवा ऑफिस की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं।
असल में इस पीढ़ी की मुख्य बात यह है कि ये जैसे हैं, वैसे ही रहना चाहते हैं। यहां तक कि ऑफिस में भी इन्हें प्रोटोकॉल फॉलो करना नहीं भाता। यह वह पीढ़ी है, जिसके पिता उसके दोस्त जैसे हैं। पिछली पीढ़ी को जो जीवन-मूल्य, सही-गलत सिखाए गए थे, वो इस पीढ़ी को उस तरह नहीं बताए जा सके हैं।
मुश्किलात कई हैं, लेकिन कई ऐसे गुण भी हैं, जो ‘जेन-ज़ी’ में खास हैं। टेक्नोलॉजी के महारथी, मल्टीटास्किंग में मंझे हुए, नेचरल या सहज रहने वाले आदि। अब इस पीढ़ी पर एक व्यापक नजर डालने और उनकी दिक्कतों को समाज कैसे संभाले, इस पर बात होनी चाहिए।
किसी कार्यक्रम, फिल्म, चैनल को बंद करना तो अतिरेक है। यह वैसे ही है, जैसे मुगल आक्रांता थे तो पाठ्यक्रम में औरंगजेब को पढ़ाना ही बंद कर दो। पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आक्रांता कैसे नुकसान करते थे। समाज को परिपक्व होने दीजिए।
इलाहाबादिया का उदाहरण अपने आप ही बाकियों के लिए सबक बनेगा।
Date: 20-02-25
ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम
कल्याणी शुक्ला, ( सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी सिक्योरिटी में रिसर्च कंसल्टेंट )
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट-भाषण की शुरुआत तेलुगु कवि गुरजाड अप्पाराव की इन पंक्तियों से की थी : ‘देश सिर्फ उसकी मिट्टी ही नहीं, उसके लोग भी हैं।’ इस वर्ष के बजट का फोकस ‘सबका विकास’ पर था, जो विकसित भारत के विजन के अनुरूप है। लेकिन इस विजन का सम्बंध ‘स्वच्छ भारत, हरित भारत’ के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताने और 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को अर्जित करने से भी है। इस वित्तीय वर्ष में रीन्यूएबल एनर्जी (आरई) के लिए किया गया बजट आवंटन भी इस पर जोर देता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। कुल परिव्यय ₹26,549 करोड़ रुपयों का होगा। पिछले वर्षों की तुलना में यह बहुत अधिक है। यह बताता है कि भारत जीवाश्म ईंधन से दूर होकर स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर निरंतर बढ़ रहा है।
2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में सौर ऊर्जा क्षमता के विस्तार पर खासा जोर दिया गया है। पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना जैसी प्रमुख पहलें इसके केंद्र में हैं। पीएम सूर्य घर के अंतर्गत लगभग दस लाख रूफटॉप प्रणालियां (आरटीएस) स्थापित की जा चुकी हैं। इस योजना को 20,000 करोड़ रु. दिए गए हैं। प्रारंभिक योजना में मार्च 2026 तक 40 लाख घरों और मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों तक पहुंचने की परिकल्पना की गई थी। इसके साथ सोलर पॉवर ग्रिड प्रोग्राम को भी 1500 करोड़ दिए गए हैं। इन पहलों को सौर सेल्स पर कस्टम ड्यूटी को 25% से घटाकर 20% करने जैसे नीतिगत उपायों से बल मिला है। सोलर पीवी सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना का रणनीतिक उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सौर ऊर्जा से जोड़ना है, जिसके लिए बजट में 2,600 करोड़ रु. का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है।
बजट का व्यापक दृष्टिकोण ग्रिड-एकीकरण में सुधार और अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन क्षमता का विस्तार करने तक फैला हुआ है। इससे बढ़ी हुई रीन्यूएबल ऊर्जा क्षमता को राष्ट्रीय ग्रिड में निर्बाध रूप से समाहित करने में सुविधा होगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी भारत के रीन्यूएबल एनर्जी बुनियादी ढांचे के विकास का महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है। इसके लिए बजट में 600 करोड़ दिए गए हैं। विद्युत प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए फंडिंग बढ़ाई गई है। हालांकि ये आवंटन सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, लेकिन इनके वर्ष-दर-वर्ष वित्तपोषण में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।
इस पहल को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) से प्राप्त आय का समर्थन प्राप्त है, जिसके तहत सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सहित विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 20,000 करोड़ जुटाए हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भारत की व्यापक स्वच्छ ऊर्जा रणनीति का अंग है, जो रीन्यूएबल एनर्जी के फैलाव को सुगम बनाएगा और ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करेगा।
ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सरकार की पहल भी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दर्शाती है। बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 600 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष से दोगुना है। पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित 535 करोड़ रुपए के साथ यह मिशन घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग को समर्थन देने के लिए बनाया गया है, जो हरित बिजली का उपयोग करके पानी से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बायो-एनर्जी कार्यक्रम के लिए भी 325 करोड़ दिए गए हैं। परमाणु ऊर्जा पर ध्यान देते हुए 2020 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। हालांकि पवन ऊर्जा के लिए आवंटन में गिरावट है।
 Date: 20-02-25
Date: 20-02-25
क्या है विकसित भारत की राह?
देवाशिष बसु, ( लेखक मनीलाइफ डॉट इन के संपादक और मनीलाइफ फाउंडेशन के न्यासी हैं )
 मौजूदा सरकार ने जब से ‘2047 तक विकसित भारत’ का नया नारा दिया है तभी से बहस-मुबाहिसे चल रहे हैं कि देश संपन्न कैसे हो। कोई देश कैसे धनवान बनता है इस पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बहस चलती रहती है। इसकी वजह यह है कि दुनिया में कुछ ही संपन्न देश हैं और उनके चारों ओर ऐसे देशों का जमावड़ा है, जो संघर्ष कर रहे हैं। विश्व बैंक ने विभिन्न देशों को निम्न आय, निम्न-मध्यम आय, उच्च-मध्यम आय और उच्च आय की श्रेणियों में बांटा है। उसके हिसाब से दुनिया में 58 देश उच्च आय की श्रेणी में आते हैं मगर उनमें आपस में बहुत अंतर हैं। उनके अलावा 28 देश उच्च आय वाले कहलाते हैं मगर हमारी इस चर्चा में उनकी जगह नहीं बनती क्योंकि उनमें नन्हे-नन्हे द्वीप, यूरोपीय रियासतें, यूरोपीय देशों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र या बेहद कम कर वाले देश (टैक्स हेवेन) शामिल हैं।
मौजूदा सरकार ने जब से ‘2047 तक विकसित भारत’ का नया नारा दिया है तभी से बहस-मुबाहिसे चल रहे हैं कि देश संपन्न कैसे हो। कोई देश कैसे धनवान बनता है इस पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बहस चलती रहती है। इसकी वजह यह है कि दुनिया में कुछ ही संपन्न देश हैं और उनके चारों ओर ऐसे देशों का जमावड़ा है, जो संघर्ष कर रहे हैं। विश्व बैंक ने विभिन्न देशों को निम्न आय, निम्न-मध्यम आय, उच्च-मध्यम आय और उच्च आय की श्रेणियों में बांटा है। उसके हिसाब से दुनिया में 58 देश उच्च आय की श्रेणी में आते हैं मगर उनमें आपस में बहुत अंतर हैं। उनके अलावा 28 देश उच्च आय वाले कहलाते हैं मगर हमारी इस चर्चा में उनकी जगह नहीं बनती क्योंकि उनमें नन्हे-नन्हे द्वीप, यूरोपीय रियासतें, यूरोपीय देशों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र या बेहद कम कर वाले देश (टैक्स हेवेन) शामिल हैं।
कॉन्गो, रवांडा, सोमालिया, मोजांबिक, यमन, अफगानिस्तान और उत्तर कोरिया समेत 26 देशों को निम्न आय की श्रेणी में रखा जाता है और नाकाम देश (फेल्ड स्टेट) कहा जाता है। उनमें से अधिकतर अफ्रीका और एशिया में हैं। भारत को निम्न-मध्यम आय वर्ग में रखा गया है, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका समेत कुल 52 देश हैं। इनके बाद 54 देश उच्च-मध्यम आय वाले हैं। संक्षेप में, छोटे द्वीपों और टैक्स हेवेन को छोड़ दें तो 70 प्रतिशत दुनिया को धनी नहीं कहा जा सकता। धनी या संपन्न देश यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा पूर्वी एशिया में ही हैं। इसका मतलब है कि कोई भी देश किसी नियम की वजह से धनवान नहीं बनता बल्कि संपन्न देश अपवाद होते हैं। क्या भारत अतीत को छोड़कर विकसित देशों की कतार में शामिल हो सकता है?
अतीत बताता है कि पिछले 80 साल में ज्यादातर देश आय वर्ग की सीढ़ी पर केवल एक पायदान ऊपर पहुंच पाए हैं। जो देश आज धनी हैं, वे 19वीं सदी की शुरुआत में ही ऐसा कर पाए हैं। हां, उन्हें इस बात का श्रेय देना होगा कि वे आज भी संपन्न बने हुए हैं। सच यह है कि जैसे पश्चिम यूरोप के देश लुढ़ककर मध्यम आय की श्रेणी में नहीं गिरे वैसे ही निम्न आय वाले देशों के लिए उछलकर उच्च आय वाली जमात में पहुंचना लगभग असंभव रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चार देश ही ऐसे रहे हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था ने इतनी तेज रफ्तार भरी और इतने लंबे अरसे तक दौड़ती रही कि वे युद्ध की विभीषिका से उबरकर खुद को संपन्न देशों की जमात में ले आए। अपने जुझारूपन की बदौलत अपनी किस्मत बदलने वाले ये देश ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर हैं।
चीन अब भी संपन्न राष्ट्र नहीं बन पाया है। वह उच्च-मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में है। उसका वृद्धि धीमी पड़ गई है और वह मध्यम आय के जाल से बचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। कुछ देश थोड़ा ऊपर उठकर उच्च-मध्यम आय वर्ग में पहुंच गए हैं, लेकिन वे विकसित कहलाने की हैसियत अभी हासिल नहीं कर पाए हैं। तो हम किस वजह से यह भरोसा कर सकते हैं कि भारत वह हासिल कर सकता है, जो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये और मेक्सिको हासिल नहीं कर पाए हैं?
फिर तेज वृद्धि की राह क्या है? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसके लिए राजकोषीय अनुशासन, व्यापार और वित्तीय उदारीकरण, निजीकरण, मुक्त बाजार तथा प्रतिस्पर्द्धी माहौल बनाने की सलाह देते हैं। वृद्धि के द्वार खोलने वाले इन तरीकों को एक साथ रखकर ‘वाशिंगटन कन्सेंसस’ कहा गया है। लेकिन इनकी राह पर चलकर संपन्नता हासिल करने वाला एक भी देश नहीं है। ‘व्हाई नेशन्स फेल’ में डरोन असमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन कहते हैं कि वृद्धि के लिए समावेशी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की जरूरत होती है, जो धन और शक्ति को कुछ ही हाथों में रखने वाली संस्थाओं से अलग होती हैं। पिछले साल इन दोनों को सिमॉन जॉनसन के साथ इनके विशिष्ट कार्यों के लिए नोबेल सम्मान दिया गया था।
इस पैमाने पर देखें तो पता चलता है कि भारत में माहौल शोषणकारी है और यहां की संस्थाएं बहुत खराब हालत में हैं, जिनसे हमारी क्षमता और संभावना कमजोर हो रही हैं। लेकिन जापान का उपनिवेश रहा दक्षिण कोरिया भी 1950 में भारत जितना ही गरीब था और उसके पास भी कोई मजबूत संस्थाएं नहीं थीं।
लेकिन वहां पार्क चुंग ही ने सैन्य तानाशाही लागू की और 25 साल में ही अद्भुत आर्थिक चमत्कार करते हुए देश का कायापलट कर डाला। और चीन, जिसने पश्चिम की तरह समावेशी संस्थाओं को बगैर ही फर्राटा भर लिया?
वास्तव में यह सिद्धांत किसी भी सूरत में उन खस्ताहाल और खराब लोकतंत्रों को व्यावहारिक रास्ता नहीं दिखाता, जहां लोकलुभावनवाद की होड़ और दबाव के कारण राज्य शोषणकारी और संस्थाएं कमजोर बनी रहती हैं।
तेज आर्थिक वृद्धि की गुत्थी सबसे अच्छी तरह सुलझाने वाला मॉडल आर्थिक राष्ट्रवाद का एक खास रूप है, जिसमें नए उद्योगों को विस्तार के लिए संरक्षण दिया जाता है, सबसे अच्छी प्रौद्योगिकी का आयात किया जाता है और निर्यात में अग्रणी बनने के लिए देश के भीतर होड़ बढ़ाई जाती है। 20वीं सदी में असाधारण वृद्धि हासिल करने वाली चारों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं – जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन – में यही एकसमान बात नजर आती है। बेहतरीन नवाचार के अलावा इन्हीं तरीकों ने 18वीं शताब्दी में इंगलैंड और 19वीं शताब्दी में अमेरिका एवं जर्मनी को शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। इस मॉडल का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व नाकाम संस्थाओं को खत्म करना है चाहे वे सरकारी हों या निजी। इस तरह बाजार में वे संस्थाएं ही रह जाती हैं, जिनमें होड़ करने की क्षमता होती है।
हकीकत यह है कि सभी देशों ने इस आर्थिक नीति को अपनाने की कोशिश की है। लेकिन अधिकतर ने इस पर आधा-अधूरा या बेदिली से अमल किया। इसीलिए वे उच्च वृद्धि दर हासिल करने में पिछड़ गए। भारत के पास औद्योगिक संरक्षण था, लेकिन 1991 तक देश के भीतर प्रतिस्पर्द्धा कमजोर या नहीं के बराबर थी, जिस कारण वह ऊंची वृद्धि दर हासिल करने में पिछड़ गया। चीन ने स्थानीय प्रशासन को बेहद होड़ करने वाला बना दिया मगर भारत ने पिछड़े इलाकों के विकास का न्यायोचित मॉडल अपनाया। भारत ने निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र शुरू तो किए मगर उन्हें उस जोश के साथ रफ्तार नहीं दे पाया, जिस तरह चीन ने उन्हें आगे बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार में तो इनमें से कई पूरी तरह जमीन पर कब्जा करने के तरीके साबित हुए। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और भारत ने विदेशी प्रौद्योगिकी के लिए अपने दरवाजे तो खोले, लेकिन स्थानीय निर्यात श्रृंखला को मजबूत करने की कोई ठोस नीति नहीं अपनाई गई।
सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी नीति एकदम सटीक नहीं हो सकती। शुरुआत में कोई न कोई खामी रह ही जाती है। असली जिंदगी में काम करते हुए हमें जवाबदेही, सच्ची प्रतिक्रिया और जरूरत के मुताबिक तेजी से सुधार की आवश्यकता होती है। विजित और पराजित इसी से तय होते हैं। भारत सरकार ने 1950 में इस्पात के कारखाने लगाए, जो सफेद हाथी बन गए। दक्षिण कोरिया ने 1968 में पोहांग आयरन ऐंड स्टील प्लांट लगाया, जिसने आगे चलकर दुनिया भर से होड़ की। भारत की नियोजित अर्थव्यस्था में जब अकुशलता और भ्रष्टाचार घुसने लगा तो सुधार नहीं किया गया, अकुशल को खत्म नहीं किया गया और बढ़िया काम को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। दुख की बात यह है कि अब भी हमें इसका कोई हल नहीं मिला है।
संबंध का स्वीकार
संपादकीय
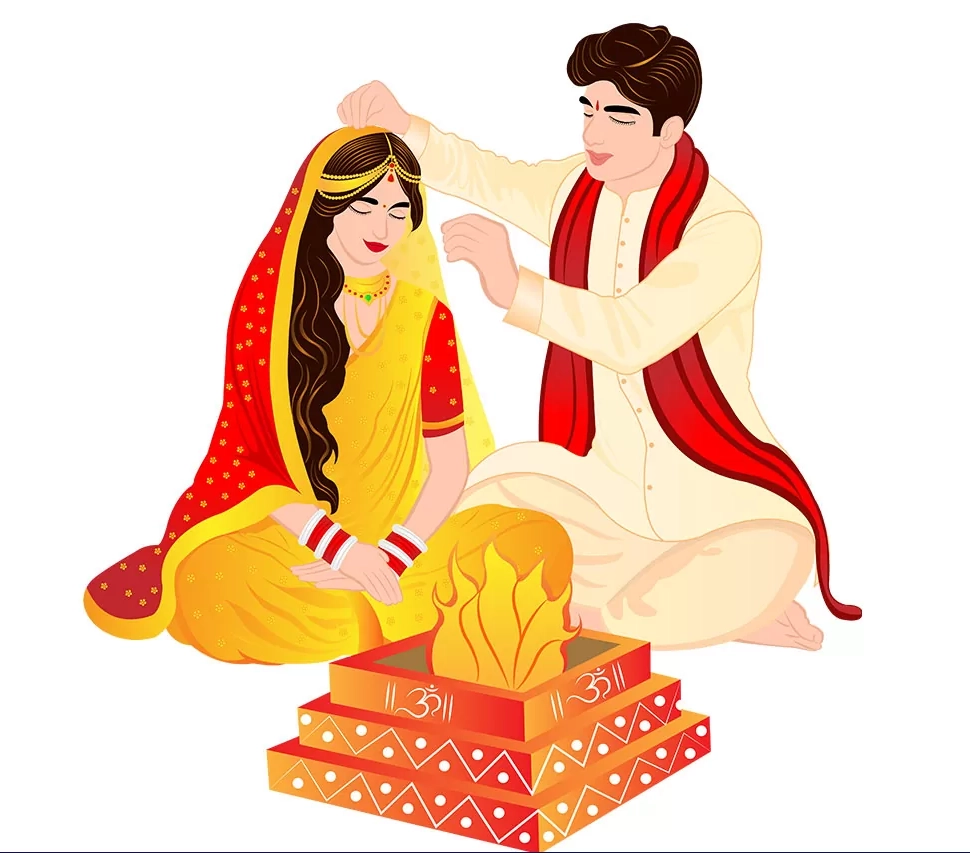 भारत में विवाह को स्त्री-पुरुष संबंध का मजबूत आधार माना जाता है। इसी से परिवार की नींव पड़ती है और हमारा समाज बनता है। इसके बरक्स अपने देश में सहजीवन को अभी तक सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। अलबत्ता, ऐसे रिश्ते चुनने वाले युगलों पर कोई वैधानिक रोक नहीं है। लोकतांत्रिक समाज की इसे उदारता कह सकते हैं। फिर भी सहजीवन के विरोध और समर्थन में प्राय: दलीलें दी जाती रही हैं। कई वर्ष पहले विवाह पंजीकरण विधेयक पारित होने के बाद भी सहजीवन को लेकर सवाल उठे थे और इसकी व्यावहारिकता पर प्रश्नचिह्न लगे थे। आखिरकार सहजीवन में रह रहे युगल भी समाज का ही हिस्सा होते हैं और जहां भी रहते हैं, वहां उन्हें सब देखते और जानते ही हैं। इस तरह उनका कुछ भी गोपनीय नहीं रहता। ऐसे ही एक युगल के तर्क पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी गलत नहीं कि जब आप विवाह किए बिना साथ रहते हैं, तो सहजीवन का पंजीकरण आपकी निजता पर हमला कैसे हुआ? आप समाज में रह रहे हैं, न कि जंगल में। इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर ऐसे किसी रिश्ते में गहरा समर्पण और एक-दूसरे पर भरोसा है, तो फिर डर कैसा?
भारत में विवाह को स्त्री-पुरुष संबंध का मजबूत आधार माना जाता है। इसी से परिवार की नींव पड़ती है और हमारा समाज बनता है। इसके बरक्स अपने देश में सहजीवन को अभी तक सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। अलबत्ता, ऐसे रिश्ते चुनने वाले युगलों पर कोई वैधानिक रोक नहीं है। लोकतांत्रिक समाज की इसे उदारता कह सकते हैं। फिर भी सहजीवन के विरोध और समर्थन में प्राय: दलीलें दी जाती रही हैं। कई वर्ष पहले विवाह पंजीकरण विधेयक पारित होने के बाद भी सहजीवन को लेकर सवाल उठे थे और इसकी व्यावहारिकता पर प्रश्नचिह्न लगे थे। आखिरकार सहजीवन में रह रहे युगल भी समाज का ही हिस्सा होते हैं और जहां भी रहते हैं, वहां उन्हें सब देखते और जानते ही हैं। इस तरह उनका कुछ भी गोपनीय नहीं रहता। ऐसे ही एक युगल के तर्क पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी गलत नहीं कि जब आप विवाह किए बिना साथ रहते हैं, तो सहजीवन का पंजीकरण आपकी निजता पर हमला कैसे हुआ? आप समाज में रह रहे हैं, न कि जंगल में। इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर ऐसे किसी रिश्ते में गहरा समर्पण और एक-दूसरे पर भरोसा है, तो फिर डर कैसा?
दरअसल, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सहजीवन का पंजीकरण अनिवार्य करने के खिलाफ एक याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है। आज की पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है कि ऐसे रिश्ते के लिए यह कानूनी व्यवस्था क्यों करनी पड़ी? ऐसा क्यों लगता है कि सहजीवन से विवाह संस्था को खतरा है। क्या कोई भी समाज परिवार बनाने और बचाने की भावना को कमजोर होते देख सकता है? वहीं स्त्रियों की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। सहजीवन में रह रहीं कई महिलाओं से मारपीट और घरेलू हिंसा के मामले सामने आने के बाद भारतीय समाज में चिंता बढ़ी है। सहजीवन में जन्मी संतानों और उनकी मांओं के कानूनी अधिकार को भी नजरअंदाज नहीं किया सकता। ऐसे में इस तरह के रिश्ते के पंजीकरण से भला क्यों परहेज होना चाहिए? यह अजीब बात है कि हम आधुनिकता की अंधी गलियों में आंखें मूंदे क्यों भटक रहे हैं।
अश्लीलता पर ‘सुप्रीम’ लताड़
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार लगाई है । समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ पर की गई रणवीर की अभद्र टिप्पणी से नाराज शीर्ष अदालत ने लताड़ लगाते हुए कुछ सवाल भी किए। अदालत ने कहा कि इलाहाबादिया के दिमाग में गंदगी थी, जिसे यू-ट्यूब शो पर उगल दिया गया। रणवीर द्वारा इस्तेमाल शब्दों ने बहन- बेटियों, माता-पिता, यहां तक कि समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराई । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है। अदालत ने यू-ट्यूबर को पासपोर्ट थाने में जमा कराना होगा, वह बगैर इजाजत देश से बाहर नहीं जा सकेगा। उसे अपने खिलाफ दर्ज शिकायतों में पुलिस जांच का सहयोग भी करना होगा । उसका शो भी अगले आदेश तक ऑन- एअर नहीं होगा। अदालत ने कहा कि समाज के स्व-विकसित मूल्य हैं, उनका सम्मान करने की जरूरत है। यू-ट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर ने परिवार, महिलाओं और मांओं के खिलाफ मसखरी के नाम पर अश्लील टिप्पणियां कीं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिसके खिलाफ देश भर में नाराजगी देखी गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी को स्त्री- विरोधी और समाज के लिए अहितकर माना । अदालत ने सरकार से भी सवाल किया कि वह कुछ करे, अगर वह अश्लील कंटेंट पर कुछ करना चाहती है तो हमें खुशी होगी। अश्लीलता और फूहड़ता के कोई मापदंड नहीं होते परंतु समाज में भाषा और बर्ताव को लेकर शालीनता बरतनी होती है। लोकप्रिय होने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने दिमाग की गंदगी सार्वजनिक रूप से उगलने का अधिकार मिल गया। सस्ता प्रचार पाने के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का अधिकार समाज में किसी को नहीं प्राप्त है। वास्तव में मजाक-मसखरी अपने समाज का अहम अंग हैं परंतु इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि कमर के नीचे प्रहार किए जाएं। सबस्क्राइबर तथा व्यूज बढ़ाने के लोभ में अक्सर यू-ट्यूबर फूहड़ता और अश्लीलता का सहारा लेते नजर आते हैं। समय रहते यदि इस तरीके पर सख्त लगाम न लगाई गई तो मसखरी-मखौल की आड़ में गाली-गलौच करने या अश्लीलता परोसने वालों को यकीनन प्रश्रय मिलता रहेगा। कलात्मकता और बोलने की स्वतंत्रता के बावजूद श्लीलता – अश्लीलता के दरम्यान की अति संवेदनशील बारीक रेखा का अहसास करना होगा । और यह स्वनियमन से हो तो और भी बेहतर।