
19-07-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 19-07-25
Make Agents of Public Dirtiness Pay
India needs disincentives and punitive action
ET Editorials

‘A lavatory must be as clean as a drawing-room. I learnt this in the West.’ No one can accuse Mohandas Gandhi of suffering from a colonial mindset. And, yet, 100 years after he shared this candid observation, and more than a decade after Swachh Bharat Abhiyan was launched, India remains a filthy society. Once that reality has been acknowledged, strategies to back up policy intent can be drawn and executed. Staggering apathy to civic sense contributes to public squalor. And this stubborn mindset is remarkably class and economy agnostic. Swachh Survekshan 2024-25 announced on Thursday has a good idea: to laud urban sanitation and public hygiene. But what is woefully lacking is punitive action against agents of public dirtiness.
Economic costs of poor sanitation as a share of GDP serve as a key marker of development. While advanced economies have achieved universal access to improved sanitation, coverage in the developing world drops to just half the population. Poor sanitation contributes significantly to the global disease burden, followed closely by productivity losses due to malnutrition. These, along with issues such as clean-up costs and impact on tourism, canamount to over 5% of GDP in developing economies.
The list of cleanest cities this year is topped by 8-time winner Indore, Surat and Navi Mumbai. In the 3-10-lakh population category Noida secured the top spot as cleanest city, with Chandigarh coming in second, and Mysururankingthird. In contrast, larger cities with legacy sanitation systems often struggle to upgrade their infrastructure. Since sanitation typically incurs a unit cost per person, the most effective approach is to integrate it into municipal budgets early and work on keeping costs low as cities grow. This results in long-term savings, particularly in clean-up expenses. But at the heart of the problem lies the paradox of citizens being obsessed with personal ‘purity’, while being blasé about public cleanliness. This can change only with strong disincentives, not just incentives like ranking clean cities.
Date: 19-07-25
All in one
Agriculture needs more public spending, not just one umbrella scheme
Editorials
The Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (PMDDKY), a scheme approved by the Union Cabinet, is to be implemented through the convergence of 36 existing schemes across II Departments. According to Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan, the scheme seeks to address the “disparities in productivity” between States, and even among districts within a State. The Centre’s pet schemes such as the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) and the PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) as well as relevant State schemes, to be identified by the District Dhan Dhaanya Samitis, will be subsumed in the PMDDKY. Local partner- ships with the private sector will also be promot ed under the proposed scheme, which will begin in October during the rabi crop season. The scheme is to get an annual outlay of *24,000 crore for six years. Modelled on NITI Aayog’s As- pirational Districts Programme, the Centre will identify 100 districts based on low productivity and cropping intensity and less credit disbursement. The hope is that the scheme will result in higher productivity, value addition in agriculture and allied sectors, local livelihood creation, leading to increased domestic production and self-reliance. This convergence of schemes must be viewed in the background of decreasing public spending on agriculture. The Parliamentary Standing Committee on Agriculture, in the latest report on Demands for Grants, had observed a continuous decline, from 3.53% in 2021-22 to 3.14% (2022-23), 2.57% (2023-24), 2.54% (2024-25) and 2.51% (2025-26), of the allocations for agricul- ture as a percentage of total Central Plan outlay.
This aggregation of all schemes under one umbrella suggests that the Government wants uniformity in running the welfare, financial and technical schemes in the agriculture sector. It is keen to add States’ measures too in the new scheme. It remains to be seen how effective such uniformity will be on the ground as further de crease in public investment in agriculture could be disastrous. Private-public partnerships should be for the larger good of self-reliance, particularly in the production of foodgrains, edible oil and pulses. The progress of area coverage under kharif crops, released last week, points to a decrease in the sowing of oil seeds and popular pulses. Though it promotes national uniformity, it is welcome that the new scheme will function based on ‘District Plans’ that will be aligned to the national goals of crop diversification, conservation of water and soil health, self-sufficiency in agriculture and allied sectors. For the PMDDKY, the Centre will monitor 117 key indicators of progress on a monthly basis. But to make it more participatory, States, local self governments, primary agriculture cooperative societies, agriculture universities and organisations of farmers and traders must be involved in this process.
Date: 19-07-25
क्या हम दुनिया में अपने उत्पाद लेकर जा सकते हैं?
संपादकीय
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार अप्रैल में भारत का अमेरिका को निर्यात 27.31% बढ़ा। अगर हमें इतना ही सत्य मालूम हो तो उत्साहित हो सकते हैं। लेकिन दूसरा तथ्य यह है कि इसी काल में न चाहते हुए भी हमारा चीन से आयात भी 27.03% बढ़ा है। ट्रम्प की टैरिफ नीति से दुनिया में पैदा हुई हलचल के बीच भारत की टैरिफ दर फिलहाल भले ही कम हो लेकिन सच यह है कि हमारे कृषि और डेयरी उत्पाद ज्यादा लागत के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खड़े नहीं हो सकते। स्टील से लेकर एल्युमीनियम और तमाम रेयर – अर्थ तत्वों के लिए (जिनके बिना हमारी मैन्युफैक्चरिंग आगे नहीं बढ़ सकती) हम चीन पर निर्भर हैं। अगर हमने अपने खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न करना पूंजी निवेश की कमजोर नीति के कारण जारी रखा तो निर्यात पर हमारी खुशी बनावटी होगी क्योंकि असली लाभ चीन का होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कृषि आधारित आबादी, सर्वाधिक पशुधन (संख्यात्मक रूप) और दूध पैदा करने दुनिया में अव्वल (240 मिलियन टन) भारत दुनिया की मंडियों में न तो डेयरी और ना ही अनाज लेकर खड़ा हो सकता है। ट्रम्प के पहले भी जब दशकों तक टैरिफ नहीं लगता था या कम लगता था तब भी क्या हमने इतना ट्रेड संतुलन अपनी ओर कर लिया था कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में सीना चौड़ा करके युवाओं को रोजगार दे सके ?

Date: 19-07-25
कॉरपोरेट जगत में विविधता जरूरी
संपादकीय
हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में प्रिया नायर की नियुक्ति देश के कॉरपोरेट जगत के लिए एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय कॉरपोरेट जगत ने नेतृत्वकारी भूमिकाओं में लैंगिक यानी स्त्री-पुरुष कर्मचारियों की संख्या में विविधता को लेकर बहुत धीमी प्रगति की है। नियामकीय मानकों मसलन सूचीबद्धता के लिए नियमों में सूचीबद्ध कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक की अनिवार्यता आदि ने कंपनियों को बोर्ड रूम में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि उतनी प्रगति नहीं हो सकी है जितनी कि अपेक्षित थी। कंपनियों के बोर्ड में महिलाएं 21 फीसदी पदों पर हैं जबकि नैशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में से केवल 5 फीसदी में ही महिलाएं सीईओ या प्रबंध निदेशक के पद पर हैं।
बहरहाल, शीर्ष पर कुछ प्रगति के बावजूद व्यापक तस्वीर अभी तक असमान बनी हुई है। मानव संसाधन सलाहकार कंपनी माचिंग शॉप्स द्वारा हाल ही में जारी ‘माचिंग शीप इन्क्लूजन इंडेक्स 20251 के अनुसार भारत की 63.45 फीसदी सूचीबद्ध कंपनियों में अभी भी महत्त्वपूर्ण पदों पर महिलाएं नहीं हैं। ऐसे हालात तब भी बने हुए हैं जबकि तथ्य बताते हैं कि समावेशन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों ने अपने समकक्षों की तुलना में अच्छा मुनाफा कमाया।
विविधता केवल नैतिकता का प्रश्न नहीं है। यह वाणिज्यिक दृष्टि से भी अहम है। अगर करीब से नजर डालें तो पता चलता है कि देश के कारोबारी क्षेत्र में लैंगिक विविधता हर तरह से असंतुलित है। शुरुआती स्तर की भर्तियों में महिलाओं का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है और वे शीर्ष पर भी नजर आती है लेकिन प्रबंधन के मध्यम स्तर पर महिलाओं की संख्या काफी कम नजर आती है। ध्यान रहे कि यही मध्यम स्तार का प्रबंधन आगे चलकर शीर्ष नेतृत्व की तरफ बढ़ता है। इतना ही नहीं, महिलाओं को अक्सर मानव संसाधन और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे क्षेत्रों में रखा जाता है जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन रणनीतिक कारोबारी निर्णयों में इनकी भूमिका अक्सर कुछ खास नहीं होती। मैकिंजी की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वित्त, परिचालन और कोर बिजनेस इकाइयों में पुरुषों का दबदबा बरकरार है। यह रझान न केवल महिलाओं की करियर वृद्धि को रोकता है बल्कि कंपनियों की निर्णय प्रक्रिया में गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। अहम कारोबारी कार्यों में लैंगिक विविधता की कमी के कारण संकीर्ण दृष्टिकोण विकसित हो सकते हैं और अवसर गंवाने पड़ सकते हैं। देश के कॉरपोरेट जगत के कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 22 फीसदी है, यह आम श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी से भी कम है। ऐसे में देश के जनांकिकीय बढ़त का पूरा लाभ लेने के लिए समावेशन को हकीकत में बदलना होगा। कंपनियां न केवल बोर्ड स्तर पर बल्कि सभी कामों में भर्ती, नौकरी छोड़ने, वेतन और पदोन्नति के संबंध में लिंग- आधारित मानकों पर नजर रखकर डेटा आधारित पारदर्शिता को अपना सकती हैं। जिस तरह बड़ी कंपनियां नियमित पर्यावरण और संचालन मानकों के अनुपालन की जानकारी देती हैं, विविधता के आंकड़े कमियों को पहचानने और लक्षित हस्तक्षेप करने में मददगार हो सकते हैं। ढांचागत मार्गदर्शन के साथ नेतृत्व विकास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें संभावनाशील महिलाओं को आगे बढ़ाना और उन्हें प्रशिक्षित करना जरूरी है। खासकर वित्तीय और परिचालन के क्षेत्र में ऐसे में अनुकूल कामकाजी माहौल बनाना आवश्यक है। समावेशी नीतियां मसलन लचीला कार्य समय, मातृत्व अवकाश और पुनप्रवेश कार्यक्रम आदि को उत्पादकता बढ़ाने में सहायक माना जा सकता है। पर्यावरण, सामाजिक और संचालन फ्रेमवर्क यानी ईएसजी की तरह विभिन्न भूमिकाओं में लैंगिक पहचान के स्वैच्छिक खुलासे को प्रोत्साहित कर नियामक भी इसमें सहायक भूमिका निभा सकते हैं। बड़े निवेशक भी अपने कॉरपोरेट संचालन और दीर्घकालिक जोखिम के मूल्यांकन में विविधता को ध्यान में रख रहे हैं। कारोबारी भारत को प्रतीकात्मक समावेशन से आगे बढ़कर वास्तविक प्रभाव की दिशा में बढ़ना होगा। इसका अर्थ यह है कि न केवल महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिका सौंपनी होगी बल्कि उन्हें प्राधिकार, संसाधन और निर्णय प्रक्रिया में भी शक्ति संपन्न बनाना होगा। इसका लक्ष्य केवल समता हासिल करना नहीं बल्कि मजबूत, नवाचारी और भविष्य की दृष्टि से सक्षम संगठनों का निर्माण करना भी है। इस प्रयास में लैंगिक संतुलन वाला नेतृत्व अहम है।
Date: 19-07-25
स्पष्ट संदेश
संपादकीय
इसमें कोई दोराय नहीं कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए सभी जरूरी विकल्पों पर काम होना चाहिए और खासतौर पर इसमें वैसे देशों को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, जो इसमें अपना कुछ प्रभाव रखते हैं। संभव है कि अमेरिका भी रूस-यूक्रेन युद्ध का अंत ही चाहता हो। मगर जिन देशों से इस युद्ध को खत्म कराने के लिए कुछ करने की उम्मीद की जा रही है, क्या धाँस या धमकी के जरिए उनसे ऐसा करा पाना मुमकिन है ? पिछले कुछ समय से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सुविधा के मुताबिक और हित में कई देशों पर शुल्क लगाने या बढ़ाने के विकल्प को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अब रूस- यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर भी बेजा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के महासचिव मार्क रूट ने बुधवार को भारत, चीन और ब्राजील को यह चेतावनी दी थी कि अगर वे रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं, तो उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
इससे पहले ट्रंप ने भी यह कहा था कि अगर यूक्रेन को लेकर जल्दी ही शांति समझौता नहीं किया गया, तो रूस से सामान खरीदने वाले देशों पर सौ फीसद तक का शुल्क लगाया जाएगा। जाहिर है, यह बहुध्रुवीय विश्व में अन्य देशों को अपनी सुविधा और नीतियों के मुताबिक फैसले लेने की आजादी और संप्रभुता पर डाला जाने वाला एक दबाव है, जिसकी दिशा अमेरिका की इच्छा के हिसाब से संचालित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भारत ने स्वाभाविक ही प्रतिबंध लगाने की धमकी के खिलाफ सख्त प्रतिक्रिया दी है। भारत ने गुरुवार को इस मामले में ‘दोहरे मापदंडों’ के प्रति आगाह किया और जोर देकर कहा कि रूस से उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हितों और बाजार की गतिशीलता पर आधारित है। दरअसल, दिसंबर, 2022 में जब रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब यूरोपीय संघ और अमेरिका ने यह उम्मीद की थी कि इस पाबंदी से रूस की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा और उसे यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म करने पर मजबूर किया जा सकेगा। मगर तब रूस से भारत और चीन ने तेल की खरीद जारी रखी और यही वजह है कि प्रतिबंध ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए।
सवाल है कि अगर नाटो और अमेरिका अन्य देशों के नीतिगत मामलों में इस स्तर पर जाकर दखल देना चाहते हैं, तो क्या यह प्रत्यक्ष रूप से दोहरे मापदंड नहीं हैं। राष्ट्रपति बनने के साथ ही ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म कराने के लिए बढ़-चढ़ कर दावे किए थे। मगर अब यह साफ है कि इस दिशा में ट्रंप की कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टै अमेरिका यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहा है। अब नाटो भारत, चीन और ब्राजील से रूस के राष्ट्रपति को फोन करके शांति वार्ता के लिए गंभीर होने को कह रहा है तो इसके क्या मायने हैं? भारत के पास अपनी ऊर्जा जरूरतें हैं, उपलब्धता के सीमित विकल्प हैं और फिलहाल जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसी के मुताबिक कदम उठाना होगा। याँ भी एक संप्रभु देश अपनी जरूरतों के मुताबिक ही अपनी दिशा तय करता है और भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है। इसके बावजूद अगर नाटो और अमेरिका की और से भारी शुल्क या फिर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी जाती है तो दरअसल यह टकराव और दबाव की वही नीति है, जिसे खत्म करने की वे इच्छा जता रहे हैं।
Date: 19-07-25
नवाचार की राह पर आगे बढ़ता भारत
जयंतीलाल भंडारी
केंद्र सरकार ने हाल ही में एक लाख करोड़ रुपए की शोध, विकास और नवोन्मेष (आरडीआइ) योजना को मंजूरी दी। यह शोध और विकास में निवेश के लिए बड़े प्रोत्साहन के रूप में है। खास बात यह भी है कि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पचास वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण अनुदान उपलब्ध कराएगा। यह कोष अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय मदद प्रदान करेगा और नवाचार के व्यावसायीकरण के लिए धन देगा। यह व्यवस्था वैश्विक भारतीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें भारत में प्रयोगशालाएं स्थापित करने की अनुमति देने की योजनागत सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण होगी।
भारत में सरकार और निजी क्षेत्र का शोध एवं विकास में निवेश लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। अभी भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शोध और विकास की हिस्सेदारी करीब 0.70 फीसद है। यह हिस्सेदारी अमेरिका, जापान और चीन जैसे देशों की दो से पांच फीसद हिस्सेदारी के मुकाबले बहुत कम है। साथ ही देश के तेज विकास के लिए भी अपर्याप्त है। इस योजना से शोध के रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों को आवश्यक जोखिम पूंजी प्राप्त होगी। योजना का दायरा ऊर्जा सुरक्षा से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और कृत्रिम मेघा (एआइ) तक होगा। पिछले साल जुलाई के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। अब आरडीआई में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के वास्ते कम या शून्य ब्याज दर पर लंबी अवधि के लिए धनराशि प्राप्त करने की सुविधा मुहैया होगी देश में शोध एवं अनुसंधान पर कंपनियों का अंशदान अमेरिका, जापान, चीन और यूरोपीय यूनियन की तुलना में बहुत कम है। ऐसे में निजी क्षेत्र में न केवल शोध, बल्कि विकास एवं नवाचार चरणों को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जो वैज्ञानिक संभावनाओं को बाजार के लिए तैयार नए समाधानों में बदल दें।
उल्लेखनीय है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्लूआइपीओ) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआइआइ) 2024 की रैंकिंग में 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने 39वां स्थान हासिल किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि जो भारत वर्ष 2015 में 81वें स्थान पर था, अब वह 39वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे भारत की प्रगति दुनियाभर में रेखांकित हो रही है। जीआइआइ 2024 के तहत भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है। भारत मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्र की दस अर्थव्यवस्थाओं में भी पहले स्थान पर है, जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) समूह में चौथे स्थान पर है भारत के प्रमुख शहर मुंबई, दिल्ली, बंगलुरु और चेन्नई दुनिया के शीर्ष सौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समूह में सूचीबद्ध है। भारत अमूर्त संपत्ति तीव्रता में वैश्विक स्तर पर सातवें स्थान पर है। यदि हम बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े अन्य वैश्विक संगठनों की रफ्ट को भी देखें, तो पाते हैं कि भारत इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी उद्योग मंडल ‘यूएस चैंबर्स आफ कामर्स’ के ‘ग्लोबल इनोवेशन पालिसी सेंटर’ द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा (आइपी) सूचकांक 2024 में भारत दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है।
निस्संदेह शोध एवं नवाचार तथा बौद्धिक संपदा की दुनिया में भारत की मजबूत स्थिति यह दर्शा रही है कि वह नवाचार का केंद्र बनता जा रहा है। भारत में शोध एवं नवाचार को बढ़ाने में डिजिटल ढांचे और सुविधाओं की भी अहम भूमिका है। देश सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात में लगातार आगे बढ़ रहा है। विज्ञान और इंजीनियरिंग स्नातक तैयार करने में भी भारत दुनिया में सबसे आगे है यहां उद्योग कारोबार तेजी से समय के साथ आधुनिक हो रहे हैं। कृषि से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए भारत ने जिस तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया, उससे वह कृषि विकास की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा है।
शोध एवं नवाचार के मद्देनजर निश्चित रूप से भारत ने कारोबारी विशेषज्ञता, रचनात्मकता और संचालन से जुड़ी स्थिरता जैसे विविध क्षेत्रों में अच्छे सुधार किए हैं। साथ ही देश में घरेलू कारोबार में सरलता, विदेशी निवेश जैसे मानकों में भी बड़ा सुधार दिखाई दिया है। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि बौद्धिक संपदा और शोध एवं नवाचार के बहुआयामी लाभ होते हैं। इनके आधार पर किसी देश में विभिन्न देशों के उद्यमी और कारोबारी अपने उद्योग-धंधे शुरू करने संबंधी निर्णय लेते हैं। विभिन्न देशों की सरकारें वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक को ध्यान में रख कर अपने वैश्विक उद्योग- कारोबार के रिश्तों के लिए नीति बनाने की डगर पर बढ़ती हैं। भारत में कृत्रिम मेघा और ‘डेटा एनालिटिक्स’ जैसे क्षेत्रों में शोध एवं विकास और नवउद्यम माहौल के चलते अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी- बड़ी कंपनियां अपने केंद्र स्थापित कर रही हैं।
भारत में ख्याति प्राप्त वैश्विक वित्त और वाणिज्य कंपनियां अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। पूरी दुनिया में ‘मेड इन इंडिया’ और ‘ब्रांड इंडिया’ की चमकीली पहचान बन रही है। इससे भारत में प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ रहा है। रोजगार के सुनहरे मौके सृजित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, शोध एवं नवाचार बढ़ने से देश में लगातार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि हो रही है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जून 2025 में 697 अरब डालर से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि सरकार बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार की अहमियत को समझते हुए इस क्षेत्र को प्राथमिकता देती दिखाई दे रही है। यद्यपि भारत के विकास में बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े तीन आधारों की बढ़ती भूमिका दिखाई दे रही है, लेकिन इन आधारों से विकास को ऊंचाई देने के लिए इस क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र का परिव्यय बढ़ाना होगा। इस समय भारत में शोध और विकास पर जिस तरह जीडीपी का करीब 0.70 फीसद ही व्यय हो रहा है, उसे रणनीति पूर्वक बढ़ाना होगा। ऐसे में हमें ध्यान देना होगा कि कोई छह-सात दशक पहले अमेरिका ने अनुसंधान पर अधिक खर्च कर सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, दवाओं, अंतरिक्ष अन्वेषण, ऊर्जा और अन्य तमाम क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने का अध्याय लिखा है।
उम्मीद करें कि तेज विकास और आम आदमी के आर्थिक-सामाजिक कल्याण के मद्देनजर दुनिया के विभिन्न विकसित देशों की तरह भारत में भी बौद्धिक समझ, शोध एवं नवाचार पर अधिक धनराशि व्यय करने की डगर पर आगे बढ़ा जाएगा। इससे जहां ‘ब्रांड इंडिया’ और ‘मेड इन इंडिया’ की वैश्विक स्वीकार्यता सुनिश्चित की जा सकेगी, वहीं स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, कारोबार, ऊर्जा, शिक्षा, रक्षा, संचार, अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगा। उम्मीद है कि देश को वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, वर्ष 2047 तक विकसित देश तथा दुनिया की नई आर्थिक महाशक्ति बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के मद्देनजर सरकार और उद्योग कारोबार जगत बौद्धिक संपदा, शोध और नवाचार की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।
Date: 19-07-25
बेहाल है युवा तबका
विवेक कुमार
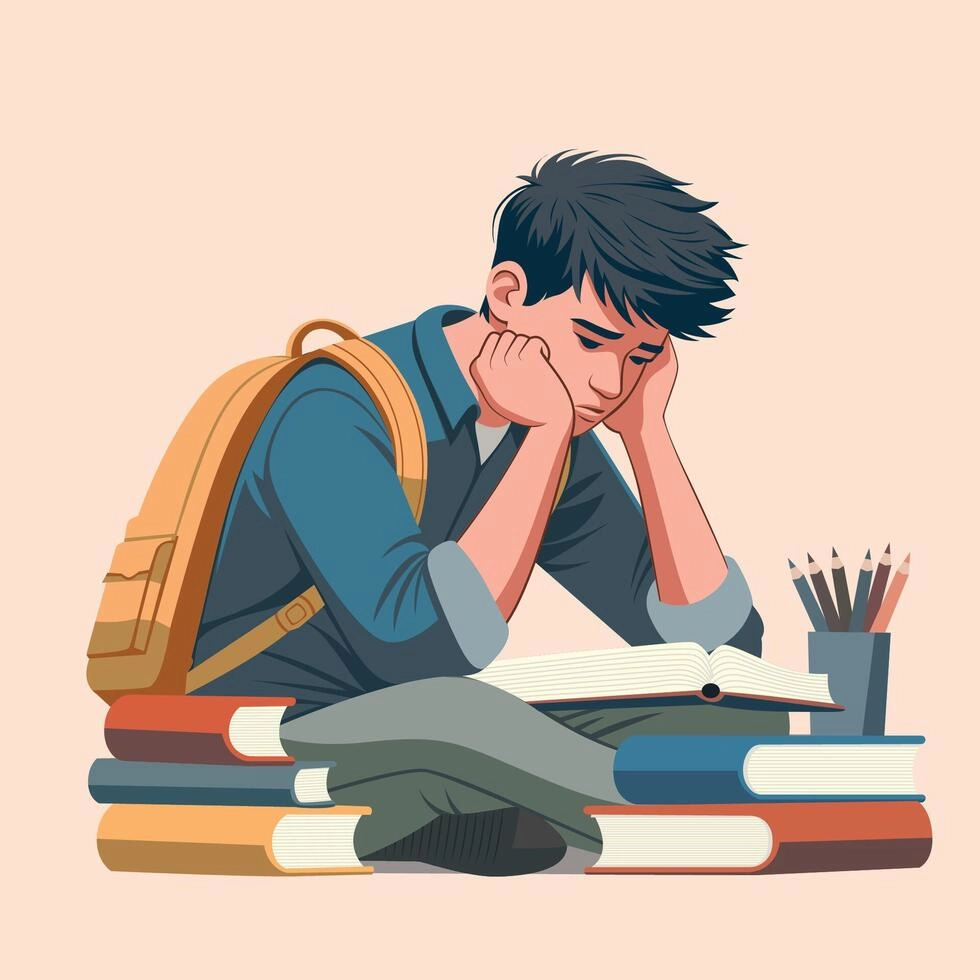
किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी वहां की युवा शक्ति होती है। युवाओं में ऊर्जा, साहस, कल्पनाशक्ति और नवाचार की क्षमता प्रबल होती है। देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास की नींव युवाओं के कंधों पर टिकी होती है। देश का युवा वर्तमान का निर्माता होता है, लेकिन इन्हीं युवाओं को समय पर सही मार्गदर्शन, संसाधन और आर्थिक मजबूती का स्रोत उपलब्ध न होने पर ये दिग्भ्रमित हो जाते हैं।
आज की युवा शक्ति अवसाद, तनाव और करियर की समस्याओं से जूझ रही है। आए दिन अखबारों की सुर्खियों में युवा द्वारा आत्महत्या करने की खबरें प्रथम पेज पर प्रकाशित होती है, मगर क्या किसी ने युवाओं की समस्याओं की जड़ तलाशने की कोशिश की है? देश का अधिकांश युवा पढ़ा-लिखा बेरोजगार है। सरकारी नौकरी की आस में घरों से कोसों दूर रह कर तैयारी करता है। ये युवा मध्यम, निम्नवर्गीय और गांव देहात से आते हैं। इनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। सरकारी नौकरी की आस में अपनी जमा पूंजी भी गंवा देते हैं। देश में हर साल लाखों युवा दिल्ली, प्रयागराज, पटना कोटा जैसे बड़े शहरों में नौकरी की परीक्षाओं के लिए तैयारी करने जाते हैं, लेकिन क्या इन सभी को सरकारी नौकरी मिल जाती है? तैयारी के दौरान इन यूवाओं को किन समस्याओं का सामना करन पड़ता है, किसी को शायद आभास न हो । लेकिन यह सत्य है कि सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वालों की तादाद बढ़ रही है जबकि सरकारी नौकरियां घट रही हैं।
पिछले कुछ वर्षों में देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। हाल में जारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक, इसी साल मई माह में कुल बेरोजगारी दर बढ़ कर 5.6 फीसद हो गई जबकि अप्रैल माह में यह 5.1 फीसद थी। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 15-29 वर्ष की आयु वर्ग वाले युवाओं में है। इसी साल अप्रैल में 15-29 वर्ष की आयु वर्ग की बेरोजगारी दर 13.8 फीसद थी जबकि 2025 मई माह में 15 फीसद हो गई है। देश में बेरोजगारी की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बेहद चिंताजनक है। 15-29 आयु वर्ग की महिलाओं में बेरोजगारी दर बीते साल अप्रैल महीने में 14.4 फीसद थी जबकि मई, 2025 में 16.3 फीसद पर पहुंच गई।
देश में पहले से आर्थिक-सामाजिक असमानताओं की शिकार महिलाएं बेरोजगारी में भी पीछे हैं। पढ़े-लिखे युवा बेरोजगार हैं। अधिकांश युवा आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के कारणों की तहकीकात करने से कई बातें स्पष्ट होती हैं। देश में युवाओं की सुनने वाला कोई नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और समय पर परीक्षाओं का न होना, परीक्षा परिणाम में देरी, समय पर भर्तियों का न आना, परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनैतिकता बढ़ रही है।
युवाओं की वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा रद्द हो जाए, या उसके परिणाम को लेकर असमंजस बना रहे, तो स्वाभाविक है कि युवा मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। वे अपने आत्मबल, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा तीनों में गिरावट महसूस करने लगते हैं। यह मानसिक तनाव धीरे-धीरे अवसाद, आत्मग्लानि और कई बार आत्मघाती प्रवृत्तियों को जन्म देता है। देश में युवाओं के बीच आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि सरकारी तंत्र की विफलता मूल कारण है। आश्चर्य की बात है कि देश में चुनाव समय पर होता है, क्रिकेट समय पर होता है, फिर प्रतियोगी परीक्षा क्यों नहीं समय पर हो रही हैं। यदि सरकार चाहे तो परीक्षा पूर्ण पारदर्शिता और निर्धारित समय-सीमा के अंदर करवा सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों को सभी स्तर की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करना चाहिए और उसी के अनुरूप परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति दी जानी चाहिए। डिजिटल तकनीक का परीक्षाओं में उपयोग करना चाहिए। सभी प्रकार के भर्ती बोर्डों की स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। परीक्षा पेपर में प्रश्नों को गलत बनाने वालों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
प्रश्नों के गलत होने पर और दोषपूर्ण विज्ञापन से कई बार भर्तियां कोर्ट में फंस जाती हैं। ऐसे में युवाओं का भविष्य गर्त में चला जाता है। युवाओं को केवल अपने को सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। खुद को नवाचार और उद्यमशीलता की दिशा में राह बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। भारत का भविष्य युवा शक्ति पर निर्भर है। यदि इस शक्ति को दिशा नहीं दी गई, तो यह भटक सकती है और अगर दिशा दी गई तो यह शक्ति देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। यह जिम्मेदारी केवल युवाओं की ही नहीं है, बल्कि सरकार, समाज और हर संस्थागत तंत्र की है कि युवाओं के सपनों की रक्षा करे, उन्हें अवसर दे और उनके संघर्ष का सम्मान करे । युवा अपने विचारों, कार्यों और सोच से समाज की दिशा तय करता है। इसलिए आवश्यक है कि राष्ट्र अपने युवाओं को उचित शिक्षा, रोजगार के अवसर और सकारात्मक माहौल प्रदान करे जिससे कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ देश की सेवा कर सकें।
