
16-06-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Code red
The push for a uniform civil code should not become a divisive tool
Editorial

A uniform civil code for the entire country is indeed a lofty goal, but the question whether introducing one for all aspects of personal law would impinge on the freedom of religion has been part of the debate. B.R. Ambedkar viewed it as desirable, but favoured its being voluntary. It is possible that a uniform code may be adopted without offending any religion, but the concept evokes fear among sections of the minorities that their religious beliefs, seen as the source of their personal laws, may be undermined. In fraught times such as the present, a common code will inevitably be seen as an imposition by the majority. Basic reforms can be given priority — such as having 18 as the marriageable age for all across communities and genders. Introducing a ‘no-fault’ divorce procedure and allowing dissolution of marriage on the ground of irretrievable breakdown, and having common norms for post-divorce division of assets were other matters the previous Commission threw up for a debate. Within each community’s laws, it will be desirable to first incorporate universal principles of equality and non-discrimination and eliminate practices based on taboos and stereotypes.
योजनाओं की प्रकृति को जाने बगैर निंदा न करें
संपादकीय
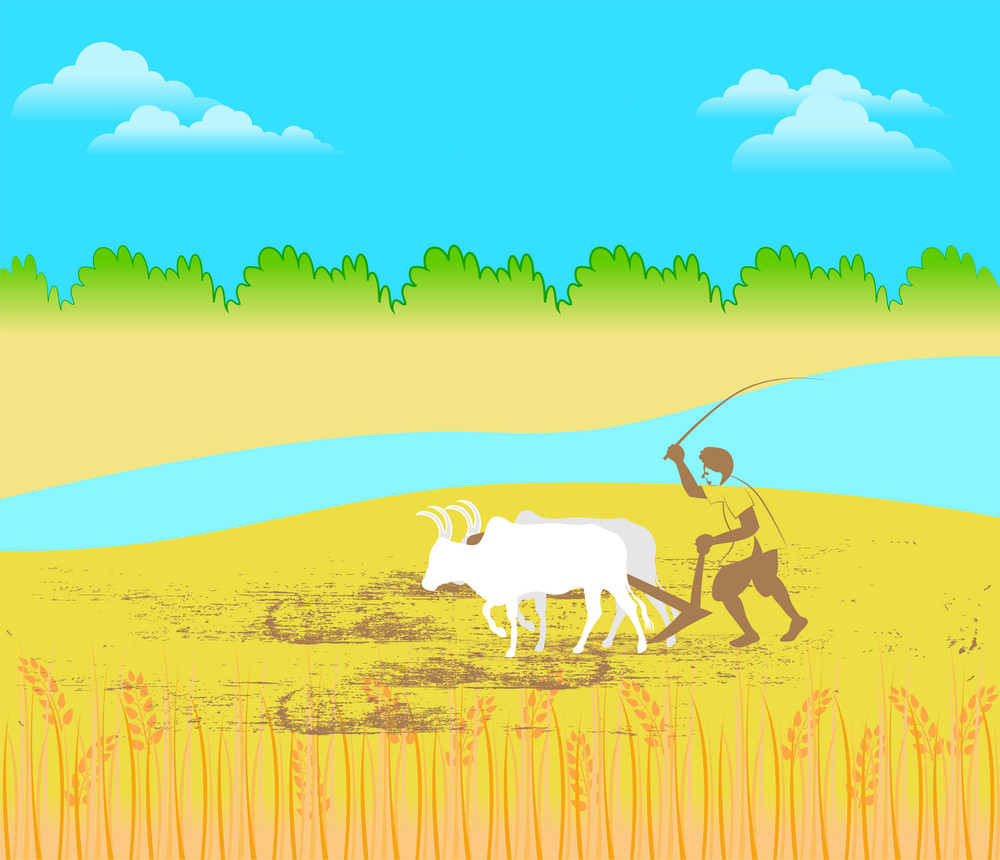
कांग्रेस अध्यक्ष सहित प्रियंका गांधी और पार्टी प्रवक्ता ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। एक दिन पहले केंद्र ने खरीफ की 17 फसलों के लिए एमएसपी में पिछले साल के मुकाबले औसत सात प्रतिशत की वृद्धि की है। इस काल में उत्पादन लागत 6.8 फीसदी बढ़ी। यानी किसान की हालत यथावत। दरअसल विपक्ष की मांग गैर-कृषि महंगाई को देखते हुए इन दरों को बढ़ाने की होनी चाहिए, पर इन नेताओं ने एमएसपी पर किसानों से कम खरीद को लेकर सरकार को घेरा है। ये शायद भूल रहे हैं कि भारत दलहन और तिलहन आयात करता रहा है लिहाजा इन उत्पादों के दाम खुले बाजार में हमेशा एमएसपी से लगभग दोगुने होते हैं। किसान दलहन की खेती से दशकों से डरता रहा है क्योंकि मौसम और बीमारी इन फसलों की दुश्मन है। इस बार हिम्मत कर किसानों ने देश की जरूरत का 90% उत्पादन किया है। कांग्रेस सहित विपक्ष की मांग होनी चाहिए एमएसपी को बाजार दरों के आसपास रखें, ताकि आढ़तिए अधिक पैदावार देखकर दरें न गिराएं। विपक्ष को यह भी समझना पड़ेगा कि एमएसपी सरकार का बाजार के दुष्प्रभावों पर अंकुश के लिए ‘हस्तक्षेप’ का तरीका है ताकि किसान हताशा बिक्री न करें। क्या विपक्ष यह समझ पाएगा ?
समान संहिता पर कुतर्क
संपादकीय
इस पर आश्चर्य नहीं कि विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता पर सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से राय मांगने की घोषणा करने के साथ ही उसके विरोध में तरह-तरह के कुतर्क दिए जाने लगे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की मानें तो समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग की पहल मोदी सरकार के ध्रुवीकरण का एजेंडा है। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि संविधान निर्माताओं ने ध्रुवीकरण के किसी एजेंडे के तहत ही अनुच्छेद 44 में यह लिखा था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है?कांग्रेस को इस प्रश्न पर विचार करने के साथ ही इस पर शर्मिंदा होना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद सबसे लंबे समय तक शासन करने के बाद भी वह समान नागरिक संहिता के मामले में संविधान निर्माताओं की इच्छा का पालन नहीं कर सकी। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि उसने ऐसा जानबूझकर किया, क्योंकि उसने तमाम विरोध के बाद भी हिंदुओं के निजी कानूनों को संहिताबद्ध कर दिया था। कायदे से तभी अन्य समुदायों के भी निजी कानून संहिताबद्ध करके समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम बढ़ा दिए जाने चाहिए थे। कांग्रेस ने ऐसा न करके देश के नागरिकों में भेद पैदा करने के साथ उन्हें अलग-अलग खांचों में बांटने का काम किया। ऐसा करके उसने राष्ट्रीय एकत्व की भावना को कमजोर किया और विभिन्न समुदायों के बीच यह आवश्यक संदेश जाने से रोका कि संविधान की निगाह में वे सभी बराबर हैं। यह खेद की बात है कि समान नागरिक संहिता के प्रश्न पर कांग्रेस अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ अपने पूर्वजों की भी अनदेखी करती है। पता नहीं क्यों वह यह भूल जाती है कि 1928 में भारत के संविधान का जो पहला प्रारूप मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था, उसमें समान नागरिक संहिता की पैरवी की गई थी? क्या इससे विचित्र और कुछ हो सकता है कि एक समुदाय के निजी कानूनों को तो संहिताबद्ध कर दिया जाए, लेकिन अन्य समुदायों को उनके निजी कानूनों के हिसाब से चलने दिया जाए और वह भी तब, जब ऐसे निजी कानून कई तरह की सामाजिक समस्याएं पैदा करने के साथ महिलाओं के हितों पर कुठाराघात करते हों?
समान नागरिक संहिता को लेकर अक्सर यह भी कुतर्क दिया जाता है कि यह सामाजिक विविधता की विरोधी है। क्या समान नागरिक संहिता अपनाने वाले अन्य देशों और विशेष रूप से अमेरिका में सामाजिक विविधता नहीं है? वहां करीब-करीब दुनिया के हर देश के नागरिक रहते ही नहीं हैं, बल्कि वहां बसने के लिए लालायित भी रहते हैं। अपने देश में भी गोवा में समान नागरिक संहिता स्वतंत्रता के पहले से ही लागू है। विरोधी दलों के नेता समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ भी कहें, यह वह विचार है, जिसके अमल का समय आ गया है।
खुशहाली से दूर होते युवा
विनोद कुमार यादव
पिछले कई वर्षों से शिक्षाशास्त्री, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री दोहरा रहे हैं कि हमारी शिक्षा-प्रणाली बहुत मशीनी होती जा रही है। अंक केंद्रित मूल्यांकन पद्धति ने विद्यार्थियों को गहरे दबाव में डाल दिया है, जिससे उनकी सहजता नष्ट हो रही है। वे बेहद चिड़चिड़े और अवसादग्रस्त होते जा रहे हैं। इस बात की तस्दीक कई शोधों और अध्ययनों के जरिए हुई है। “इटली की खूबसूरत वादियों में खुद को तलाश रही हैं शहनाज गिल” महिलाएं क्यों नहीं फोड़ती हैं नारियल, जानिए क्या है मान्यता” “फेफड़ों को साफ करने के लिए ट्राई कर सकते हैं ये 5 आसान उपाय” “मियामी में मां संग निया शर्मा की मस्ती, तस्वीरें वायरल” कुछ अरसा पहले शिक्षा मंत्रालय ने संसद में पेश एक रिपोर्ट में कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली की वजह से ग्यारह से सत्रह वर्ष आयु-वर्ग के किशोर हताशा और उच्च मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। बहरहाल, युवा वर्ग में तेजी से फैल रही इन मानसिक व्याधियों से मुक्ति के लिए प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) ने ‘हैप्पीनेस आफ साइंस’ में पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया है। फिलहाल इसकी शुरुआत संस्थान में एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर की गई है। गौरतलब है कि विश्व खुशहाली सूचकांक यानी ‘वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स’ रिपोर्ट-2023 के मुताबिक 137 देशों की सूची में भारत एक सौ पच्चीसवें स्थान पर है। यानी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद, खुशहाली के मामले में हम 124 देशों से पिछड़े हुए हैं।
आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा कहते हैं कि ‘हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशी चाहता है, मनुष्य जीवन का मकसद ही खुश रहना है। पर रोजमर्रा की भागदौड़ में हम अपने लिए एक घंटा भी नहीं निकाल पाते। आखिरकार खुशी के अहसास से वंचित ही रह जाते हैं।’ दलाई लामा का कहना है कि मन की शांति और खुशी सिक्के के दो पहलू हैं, यानी एक-दूसरे के पूरक हैं। उनका यह भी मानना है कि जब हम दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल देते हैं तो हमारे मन में शांति और हृदय में खुशी स्वाभाविक रूप से उपजती है।
सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ‘एप्पल’ का विशाल साम्राज्य स्थापित करने वाले स्टीव जाब्स ने आखिरी दिनों में मृत्यु शैया पर कहा था, ‘पूरी जिंदगी इस बेशुमार दौलत को अर्जित करने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की, व्यापार जगत की नई बुलंदियों को छुआ, किंतु खुद को संतुष्ट करने के लिए यानी अपने लिए समय निकालना जरूरी नहीं समझा। आज मौत के इतना करीब पहुंचकर वे सारी उपलब्धियां फीकी लग रही हैं। जिंदगी के आखिरी क्षणों में मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि जीवन को भरपूर आनंद से जीना चाहते हो तो हर पल खुद से प्यार करो और उन सामाजिक कार्यों में सदैव सलंग्न रहो, जिनको करने से आपको आंतरिक खुशी मिलती हो।’
खुशी का संबंध इससे नहीं है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में भौतिक संसाधन हैं या अथाह धन-संपदा है। बल्कि खुशी एक आंतरिक अवस्था है, यानी खुशी का सीधा संबंध हृदयचक्र से है। विभिन्न परिस्थतियों में या तो हम अति-उत्साहित नजर आते हैं या फिर उदास हो जाते हैं। खुशी की अनुभूति के लिए तमाम भावनात्मक परिस्थतियों के प्रति द्रष्टा भाव का बारंबार अभ्यास बेहद जरूरी है। इसके लिए सचेतनता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और कारगर गतिविधि है। सचेतनता पूरी तरह ध्यान तो नहीं, किंतु ‘ध्यान’ के करीब की एक सहज प्रक्रिया है। इसका संबंध किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति या वर्ग से नहीं है। यह मन-मस्तिष्क को बेचैन करने वाले असंख्य विचारों को शांत करने का अभ्यास है।
जब व्यक्ति का हृदय प्रफुल्लित होता है तो उसकी तरंगें मन के माध्यम से बाहर की ओर परावर्तित होने लगती हैं। असल में खुशी एक भावनात्मक अवस्था है, जिसका स्रोत हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है। आर्थिक समृद्धि की अपेक्षा व्यक्ति की खुशी उसके भावनात्मक बदलाव पर अधिक निर्भर करती है। तमाम भौतिक संसाधन और ऐश्वर्य न होने के बावजूद अगर व्यक्ति के मन में शांति है, अपनी दिनचर्या के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच है तो उसका जीवन खुशियों से परिपूर्ण है।
गौरतलब है कि हर साल सयुंक्त राष्ट्र की ओर से जारी की जाने वाली ‘वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स’ रिपोर्ट में भी अमीरी और भौतिक सुविधाओं का आकलन खुशी के संदर्भ में नहीं किया जाता। हाल ही में जारी यूएन की खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट में, जिसमें दुनिया के 137 देशों को शामिल किया गया। कोरोना महामारी की दुश्वारियों के बावजूद लगातार छठी बार उत्तरी यूरोप के देश फिनलैंड को विश्व का सबसे खुशहाल देश चुना गया। मनोविश्लेषकों की राय है कि हमारे देश में लोग पारस्परिक व्यवहार में पारदर्शिता के बजाय बौद्धिक चतुराई का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, फलस्वरूप आंतरिक खुशी के अहसास से वंचित रह जाते हैं। इसके उलट फिनलैंड के निवासी आपसी व्यवहार में ईमानदारी बरतते हैं। फिनलैंड के लोगों की खुशी शांति, संतोष और सामाजिक सुरक्षा पर आधारित है। यहां के लोगों का क्षमाशीलता में अटूट विश्वास है। असल में क्षमाशीलता ऐसा सद्गुण है, जिसके व्यावहारिक प्रयोग से हृदय में दीर्घकालिक खुशी का अहसास होता है।
जरूरी नहीं कि अरबपतियों से भरा देश खुशहाली से परिपूर्ण हो। विश्व के महाबली समझे जाने वाले अमेरिका का स्तर भी खुशहाली के लिहाज से अच्छा नहीं है। इस सूची में वह पंद्रहवें पायदान पर है। वहां सिर्फ आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। वास्तव में खुशहाली मापने के लिए आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा, पारस्परिक सहयोग और सहृदयता, शिक्षा की गुणवत्ता, मानसिक स्वास्थ्य, सामुदायिक सौहार्द, कर्तव्यनिष्ठा तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे कारकों पर विशेष ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है।
विश्व में ‘खुशहाली दिवस’ का आगाज सर्वप्रथम भूटान द्वारा किया गया। भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जिसने जीडीपी के पीछे भागती-दौड़ती दुनिया को बताया कि खुशहाली का पैमाना ‘सकल घरेलू उत्पाद’ नहीं, बल्कि ‘सकल राष्ट्रीय खुशहाली’ है। खुशी को आत्मसात करने में भूटान के नागरिकों ने मिसाल कायम की है। वे यथार्थवादी और मिलनसार हैं, वे बड़ी कामयाबी हासिल करने की एवज में छोटी-छोटी खुशियों के पड़ावों को नजरअंदाज नहीं करते। भूटान के लोगों का विश्वास है कि जो दूसरों के प्रति सदैव करुणा और मंगल-मैत्री का भाव रखते हैं, उनका हृदय क्षोभ और विषाद से मुक्त रहता है। यहां के लोग आत्मीयता और प्रेम को वरीयता देते हैं। अतीत पर पश्चाताप और भविष्य का भय छोड़कर वर्तमान का आनंद लेना ही भूटानवासियों के जीवन का मूलमंत्र है।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ‘वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट’ के सह-संपादक जान हैलीवेल का कहना है कि किसी भी देश के नागरिकों के पारस्परिक विश्वास, उदारवादी सोच और मददगार स्वभाव का खुशहाली से सीधा संबंध है। फिनलैंड और भूटान के लोगों में ये तमाम गुण अन्य देशों की बनिस्पत ज्यादा मिलते हैं। फिनलैंड की यूनिवर्सिटी आफ हेलसिंकी के मनोवैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि खुशहाली के लिए आपसी भरोसा, दूसरे के हितों को तरजीह देना और उदारता सबसे अहम है। दिलचस्प बात यह है कि फिनलैंड में आप्रवासी और अजनबी भी उतने ही भरोसेमंद हो जाते हैं, जितने कि वहां के मूल निवासी।
खुशी एक भावदशा है, जिसका स्रोत हर व्यक्ति के भीतर है। हम खुश रहना इसलिए भूल गए हैं, क्योंकि अपनी खुशी को दूसरे पर निर्भर कर दिया है। मसूरी-नैनीताल में घूमने, पांचसितारा होटल में भोजन करने, महंगी गाड़ी होने के बाद भी रात को सुकून भरी नींद नहीं आती। अगर धन-दौलत, शानौ-शौकत का तामझाम न होने के बावजूद अगर आपके पास शांति भरी आरामदायक नींद है, सुबह उठते ही उत्साह और उमंग भरी दिनचर्या है, विवेकशील और रचनात्मक नजरिया है, बेहतरीन सामाजिक संबंध है, पड़ोसियों का प्यार है तो आपसे खुशनुमा जीवन किसका हो सकता है।
समान संहिता की ओर
संपादकीय
भारत में चार वर्ष बाद फिर समान नागरिक संहिता पर विचार-विमर्श का आधिकारिक सिलसिला शुरू हो गया है, तो यह प्रत्याशित ही था। इस संहिता के संबंध में देश के किसी भी नागरिक को अपने विचार पेश करने का अधिकार है और 30 दिन के अंदर लोग विधिवत अपनी सलाह दे सकते हैं। विधि आयोग की यह पहल विचारणीय ही नहीं, बल्कि बहुत चर्चित भी रहने वाली है। भारतीय संविधान की रचना के समय से ही समान नागरिक संहिता का विषय संवेदनशील रहा है। संविधान सभा में भी उम्मीद जताई गई थी कि शायद कोई दिन ऐसा आएगा, जब देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। जब संविधान की रचना हो रही थी, तब भी अनेक लोग थे, जो समान नागरिक संहिता को कड़ाई से बनाने और लागू करने के पक्ष में थे, मगर तब के ज्यादातर नेताओं ने इस विषय पर संयम का पक्ष लिया था। बाद के वर्षों में भी बीच-बीच में समान नागरिक संहिता पर संसद या विधानसभाओं में भी खूब चर्चा हुई है। अभी चार साल पहले 2018 में भारत के विधि आयोग ने ही एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिसमें समान नागरिक संहिता को न तो आवश्यक है और न ही इस स्तर पर वांछनीय माना गया था।
यह उचित ही है कि सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से भी सुझाव देने के लिए कहा गया है। आयोग को बहुमत और नागरिक संहिता की तार्किकता पर ज्यादा गौर करना होगा। संहिता बना देना ही काफी नहीं होगा, इसे कैसे लागू किया जाएगा और कैसे सभी को साथ लेकर हम चलेंगे, इस पर भी हमें अभी से विचार कर लेना चाहिए। देश में विगत वर्षों में जो बदलाव दिखे हैं, उनकी रोशनी में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार रायशुमारी के नतीजे अलग आ सकते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में विधि आयोग ने पहल शुरू की है। वास्तव में, साल 2016 में समान नागरिक संहिता के लिए कोशिशें तेज हो गई थीं। अब चूंकि एक साल के अंदर आम चुनाव सहित अनेक राज्यों में चुनाव होने हैं, तो यह विषय गरम रहने की पूरी संभावना है। क्या कोई जल्दी है कि विधि आयोग विचार की प्रक्रिया को 30 दिन में समाप्त करना चाहता है? गौरतलब है, भाजपा के तीन बुनियादी वादे थे, राम मंदिर निर्माण, समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 370 को हटाना। इनमें से एक ही बड़ा वादा बाकी है और इसके लिए आई नई तेजी सबका ध्यान खींच रही है।
यह दलील पुरानी है कि व्यक्तिगत कानूनों में भेदभाव और असमानता को दूर किया जाए, ताकि देश में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो। किसी की भी स्थिति विशेष न रहे, सब एक समान नागरिक संहिता के तहत ही आचरण करें। इससे देश में सद्भाव और एकता का परिवेश बन सकता है। विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार संबंधी समानता की मांग पुरानी है। लगे हाथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अक्तूबर 2022 में एक हलफनामे के माध्यम से केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानून राष्ट्र की एकता का अपमान है। समान नागरिक संहिता के जरिये विभिन्न समुदायों को साझा मंच पर लाकर भारत का एकीकरण आसान होगा। कुल मिलाकर, वर्तमान शासन की मंशा स्पष्ट है, पर बहुमत का आदर और अल्पमत की चिंता के बीच समन्वय बिठाते हुए आगे बढ़ने में ही राष्ट्र की भलाई है।