
14-09-2022 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:14-09-22
Date:14-09-22
Lessons From Gyanvapi
Courts cannot offer solutions to all religious disputes. Communities must work out compromises
R Jagannathan, [ The writer is editorial director, Swarajya magazine ]
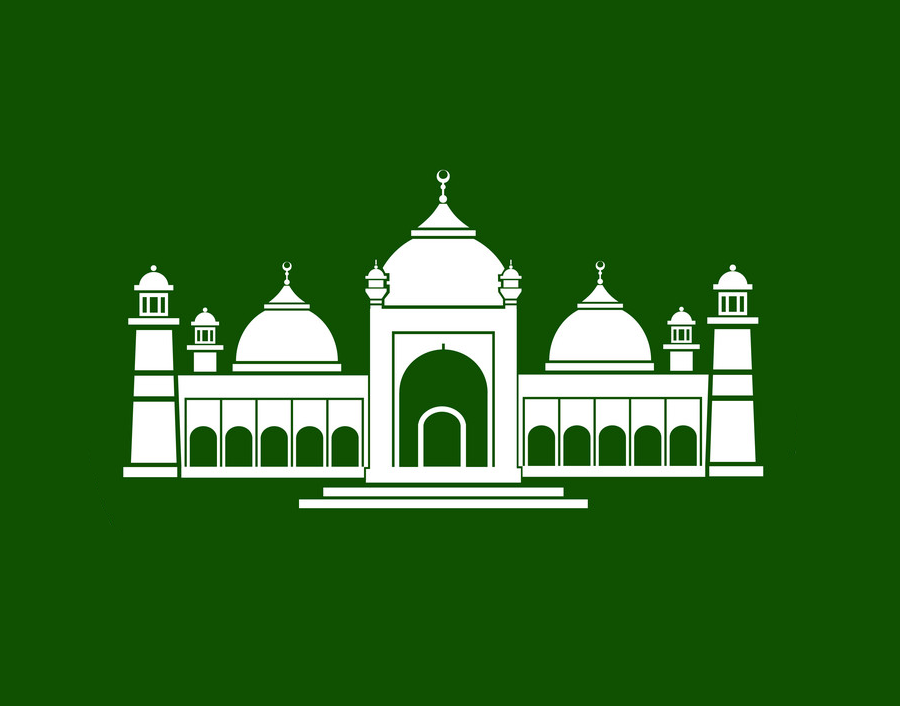
The conclusion one should draw from this “win” for one side and “loss” for the other is that much more than just legal points are involved. When communities as a whole feel aggrieved for reasons related to religious emotion, legal remedies are suboptimal.
The only real solution is for the communities themselves to work out reasonable compromises based on give and take, and this implies that most “secular” politicians – and even some “secular” historians – may not be able to help. They have anyway discredited themselves by taking partisan positions in the past.
But before we start looking for solutions, let us briefly outline the import of the initial orders of the court. District judge AK Vishvesha upheld the maintainability of the Hindu suit because:
● First, it did not ask for any change in the status of the land on which the mosque stands, and hence does not violate the Places of Worship Act, 1991, which freezes the status of religious places as they existed on August 15, 1947.
● Second, it did not contravene Section 85 of the Waqf Act, 1995, which bars civil courts from entertaining legal proceedings against Waqf property.
● And, third, it did not fall foul of the UP Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983.
However, since the right to pray to Shringar Gauri (if finally upheld) implies enhanced access to Hindus to the mosque site, the Muslim side is not going to allow the hearings to begin without more challenges in higher courts. They might well believe that once the camelgets its nose into the tent, it will only be a matter of time before they themselves are ousted from the mosque. After all, the Hindu side is widely expected to up its demands and ask for the right to worship the Shivling allegedly found in the Wuzu pond.
While the Gyanvapi dispute is in its initial stages, we need to learn a broader lesson from the Shri Ram Janmabhoomi case. Religious disputes can be endless, and even after resolution, tensions will remain. This means lasting solutions must be found through out-of-court compromises. The very fact that a legal dispute, begun as far back as the late 1940s, took nearly seven decades to achieve finality tells us that even courts will not want to get too involved.
In the Ayodhya case, two chief justices, JS Khehar in 2017, and Ranjan Gogoi in 2019, sought out-of-court settlements before the latter reluctantly decided the case with a five-judge bench. Hindus may have gotten themselves a Ram temple, but Hindu-Muslim relations remain more strained thanever.
But each legal settlement opens another can of disputes.
● Ayodhya was “resolved” in November 2019, but legal battles over Kashi and Mathura began in earnest soon after that.
● In Ahmedabad, there are Hindu claims over the Jama Masjid, which was supposedly built over the ruins of a temple.
● In Karnataka, the Guru Dattatreya Peetha/Baba Budhangiri Dargah in Chikmagalur, to which both Hindus and Muslims lay claim, remains a sore issue between the two communities despite a Karnataka HC decision of 2018 that allowed a Hindu priest to enter the shrine and offer “teertha” to all devotees, whether Hindu or Muslim. If real solutions lie with communitybased national, regional and local negotiations and compromises, the next question that arises is who can take the initiative, since all political parties have their own vote banks to cater to, and even “secular historians” and public intellectuals are badly polarised on these issues.
A tentative answer could be that a start can be made by the Sangh Parivar, Muslim religious organisations, and former SC and HC judges and civil servants from both communities. A caveat: judges and civil servants should not have been tainted by post-retirement political affiliations.
A dialogue started at the national level, and which makes progress, will cool down temperatures and set the agenda for improved inter-community relations, without which India’s economic hopes of achieving a middle-income status over the next decade will be seriously jeopardised. No country that is at war with itself can grow at the optimum level of its economic capabilities.
Three things can be attempted.
● First, setting up of a permanent History, Truth and Reconciliation Commission manned by judges or public intellectuals of impeccable honesty and credibility. Based on this consensus, history books can be rewritten.
● Second, there must be a judicialconsensus on how to deal with intra-community issues, whether it is triple talaq, Sabarimala or female genital mutilation. How far will the Constitution intervene in religious affairs to determine what is essential practice, and what is secular, and what violates basic human rights?
● Third, the tendency of the state to take over temples – and only temples – is clearly ultra vires of the Constitution in spirit, if not its letter. Temples must be returned to devotees, possibly with a separate law governing them to prevent any entry-related discrimination.
At the community level, we need dialogue and compromise; at the legislative and legal levels, we need clarity on where the law stops and where religious rights begin.
Part of a pattern
Courts should be wary of giving a toehold to communal forces in religious disputes
Editorial
Hindu revanchism has found a way to use the legal route to record early success in its latest communal campaign. The district court in Varanasi has rejected objections to the maintainability of a suit filed by five Hindu devotees seeking the right of daily worship at a spot in the Gyanvapi mosque. Of particular significance is that the court ruled that the suit is not prohibited by the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991, which freezes the status of places of worship as it was on August 15, 1947 and bars suits that seek to change their character. On the fact of it, the ruling only paves the way for the suit to be heard and is in consonance with law. The plaintiffs have argued that the spot had the status of a Hindu temple on that day and ever since, and that the suit does not seek to convert a mosque into a temple; on the other hand, they are only demanding the right to worship deities in the complex. If limited to this assertion of a religious and customary right, the suit may indeed not be barred by the 1991 law. However, it is a matter of concern that the ruling is also grounded in other claims that appear to question the mosque’s status. For instance, the court says records produced by the Anjuman Intezamia Masjid Committee were not enough to show that the complex was Waqf property. This appears in concert with the Hindu side’s claim that Muslims were “encroachers”, an assertion that clearly makes it a dispute aimed at converting the property’s status.
Courts should be wary of underhand designs behind the legal facade that such litigation builds to gain a toehold right that can be incrementally expanded. The mere pendency of some kinds of religious disputes can contribute to the vitiation of peace and harmony. It is now clear that the enactment of a special law to freeze the status of places of worship and prohibit litigation over inter-religious disputes over their location has not stemmed the Hindu right-wing’s obsession with targeting mosques and stoking communal passions. It is no surprise that the latest efforts to raise civil and legal disputes involving the Gyanvapi Mosque in Varanasi and the Shahi Idgah Mosque in Mathura are being made in tandem with a campaign against the Places of Worship Act. Several petitions have been filed challenging its validity. That such a campaign goes on despite the experience of communal frenzy through the 1990s shows the unregenerate nature of majoritarian forces. The abominable destruction of the Babri Masjid in Ayodhya, the communal riots that took place in its aftermath, the serial bomb blasts in Mumbai, and the fundamentalist violence that the sequence of events spawned cannot be forgotten. It is unfortunate that an atmosphere has been created in which the political leadership can encourage divisive litigation and exploit the process, if not influence the outcome.
मुफ्त बिजली देने की होड़
संपादकीय
रेवड़ी संस्कृति पर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहस के बीच चुनाव वाले राज्यों में जिस तरह मुफ्त बिजली देने की घोषणाएं हो रही हैं, वे बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण ढांचे को कमजोर करने के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाने वाली हैं। यह चिंताजनक है कि मुफ्त बिजली देने के वादे एक ऐसे समय किए जा रहे हैं, जब न तो राज्य बिजली बोर्डों का घाटा थम रहा है और न ही बिजली वितरण कंपनियों पर इन बोर्डों की देनदारी कम हो रही है। इस स्थिति के बाद भी इसमें संदेह है कि उन राजनीतिक दलों पर कोई असर पड़ेगा, जो चुनावी लाभ हासिल करने के लिए मुफ्त बिजली देने के वादे करने में लगे हुए हैं।चूंकि जब कोई एक राजनीतिक दल मुफ्त बिजली देने का वादा करता है तो अन्य दल भी ऐसे वादे करने के लिए विवश हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी मुफ्त या रियायती बिजली देने की मांग होने लगती है। पिछले दिनों तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने यह घोषणा कर दी कि यदि 2024 में गैर भाजपा सरकार बनी तो देश भर के किसानों को बिजली के साथ पानी भी मुफ्त दिया जाएगा। हालांकि अभी विपक्षी एकता का अता-पता नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर राव की घोषणा यही इंगित करती है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मुफ्त बिजली देने पर और जोर दिया जाएगा।
समस्या केवल यह नहीं कि एक के बाद एक राजनीतिक दल मुफ्त बिजली देने का वादा करने में लगे हुए हैं, बल्कि यह भी है कि वे इसके औचित्य को इसके बाद भी सही ठहराने में लगे हुए हैं कि इससे बिजली बोर्डों की हालत और अधिक खस्ताहाल हो रही है। निःसंदेह निर्धन-वंचित वर्गों को रियायती मूल्य पर बिजली देना समझ आता है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि सक्षम लोगों को भी लागत से कम मूल्य पर या फिर मुफ्त बिजली दी जाए।जब भी कहीं मुफ्त बिजली दी जाती है तो उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। अक्सर यह बिजली चोरी या फिर घरेलू बिजली के व्यावसायिक इस्तेमाल के रूप में सामने आता है। हालांकि सभी राजनीतिक दल इससे अवगत हैं कि अतीत में जिन राज्यों ने मुफ्त बिजली देने का काम किया, वे किस तरह मुश्किलों से घिरे, फिर भी वे चेतने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे कुछ राज्यों के बिजली बोर्डों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई कि वे बिजली की सामान्य आपूर्ति करने में भी सक्षम नहीं रहे। जिस तरह राज्यों के बिजली बोर्ड घाटे से नहीं उबर पा रहे हैं, उसी तरह बिजली वितरण कंपनियां विद्युत उत्पादक कंपनियों को समय पर भुगतान नहीं कर पा रही हैं। एक आंकड़े के अनुसार बिजली वितरण कंपनियों की देनदारी एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
 Date:14-09-22
Date:14-09-22
भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बढ़ती जटिलताएं
अजित बालकृष्णन, ( लेखक इंटरनेट उद्यमी हैं )

मुझे लगता है कि ऐसी बहसों का होना बहुत जरूरी है। भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था मोटे तौर पर ब्रिटिश युग में तैयार की गई और इसलिए इसमें बुनियादी रूप से ज्ञान को कौशल से श्रेष्ठ मानने पर ब्रिटिशों का जोर भी हमें विरासत में मिला। ऐसे में सर्वाधिक बुद्धिमान और योग्य बच्चे जिनमें परीक्षा में अधिक अंक पाने की काबिलियत होती है, वे इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा ऐसे ही अन्य तकनीकी करियर में शामिल हो जाते हैं और जिन बच्चों को ऐसी परीक्षाओं में कम अंक मिलते हैं लेकिन वे ऐसे ही तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना चाहते हैं वे पॉलिटेक्नीक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों आदि में दाखिला ले लेते हैं।
ऐेसे में आश्चर्य नहीं कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाई करने वाले बच्चों को नियमित विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने वालों की तुलना में कमतर माना जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी मैं अपने मित्रों को बताता हूं कि जर्मनी में चीजें एकदम अलग हैं तो उनके चेहरे पर असमंजस के भाव होते हैं। जर्मनी में 19 से 24 आयुवर्ग के 75 प्रतिशत लोग औपचारिक रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण लेते हैं जबकि भारत में यह आंकड़ा केवल पांच फीसदी है। भारत में एक और दिलचस्प कारक है जिसे मैं भी समझ नहीं पाया हूं: ट्यूशन क्लासेस की केंद्रीय भूमिका। फिर चाहे यह स्कूल के स्तर पर हो या किसी तरह के पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए।स्कूल के स्तर पर तथा कॉलेज के स्तर पर ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों को मनोवांछित संस्थान में दाखिले की दृष्टि से तथा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिहाज से बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी निजी ट्यूशन कक्षाएं लगभग हर जगह होती हैं और शहरी और ग्रामीण स्कूलों तथा सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी स्कूलों में बहुत मामूली अंतर है। यहां तक कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे भी ट्यूशन लेते हैं।
दक्षिण भारत के राज्यों में इसका प्रतिशत कम है जबकि पूर्वी राज्यों में दोतिहाई या उससे अधिक स्कूली बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। अधिकांश मामलों में ये बच्चे रोज ट्यूशन पढ़ते हैं। शोधकर्ताओं ने यह पता लगाने के कई प्रयास किए कि आखिर ट्यूशन को लेकर इतना आकर्षण क्यों है तो पता चला कि आमतौर पर खराब शिक्षण को इसकी वजह माना जाता है लेकिन इसकी सबसे आम वजह यह है कि चूंकि बाकी बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए लोग अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं। भारत में यह आम मान्यता है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक पाने के लिए निजी ट्यूशन जरूरी है।
क्या ट्यूशन में आपको कौशल या ज्ञान सिखाया जाता है? जहां तक मैं कह सकता हूं, ट्यूशन आपको पूछे जाने वाले संभावित सवालों के बारे में अनुमान लगाने में मदद करते हैं और आपको उनके उचित जवाब देने का प्रशिक्षण देते हैं। वास्तविक प्रश्न है: क्या इससे ज्ञान हासिल होता है?ज्यादा दिक्कतदेह बात यह है कि पिछले दशक में स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल निवेश को लेकर बढ़े उत्साह के बीच ऐसे निवेश का बड़ा हिस्सा तथाकथित एडटेक क्षेत्र में गया। इस क्षेत्र में जहां ज्यादातर कंपनियां ऑनलाइन शिक्षा को सरल ढंग से पेश करने की बात करती हैं, वहीं मूलरूप से ये परीक्षाओं की तैयारी कराने पर केंद्रित हैं। ऐसी स्टार्टअप को जो भारी भरकम मूल्यांकन हासिल हो रहा है उसे देखते हुए ऐसा लगता है मानो भारत में बच्चों के माता-पिता रुचि लेकर अपनी मेहनत की बचत को बच्चों के लिए ऐसी स्टार्टअप में लगा रहे हैं।
परंतु भारत में हम राजस्थान के कोटा जैसे संस्थानों पर नजर भी नहीं डालते जहां हर वक्त कम से कम एक लाख बच्चों को आईआईटी की प्रवेश परीक्षा निकालने की तैयारी कराई जाती है। करीब 10 लाख बच्चे इस परीक्षा में उतरते हैं और 10,000 सफल होते हैं। या देश भर में मौजूदा कोचिंग कक्षाएं जहां करीब पांच लाख बच्चे सिविल सेवा परीक्षाओं के 1,000 पदों की तैयारी करते हैं। या फिर नैशनल लॉ स्कूल की साझा प्रवेश परीक्षा जिसमें 75,000 से अधिक आवेदक 7,500 सीटों के लिए आवेदन करते हैं।अच्छी हैसियत वाले लोग अपने बच्चों को इस तरह की प्रतिस्पर्धा से बचा लेते हैं और 25 लाख रुपये से अधिक शुल्क देकर उन्हें निजी विश्वविद्यालयों में दाखिल कराते हैं या फिर चार साल की पढ़ाई के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च करके उन्हें विदेश भेज देते हैं।
हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने निजी और मुनाफा कमाने वाले कारोबारों को केजी से लेकर कक्षा नौ तक ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाने से रोक दिया। इन नए दिशानिर्देशों में साफ कहा गया है कि प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्यूशन देने वाली सभी कंपनियों को खुद को गैर लाभकारी संस्था के रूप में पुनर्गठित करना होगा। दिशानिर्देश ऐसे कारोबारों को सप्ताहांत, अवकाश के दिन तथा गर्मियों और सर्दियों की छुट्टी में भी कक्षाएं आयोजित करने से रोकते हैं। यानी सभी तरह की पढ़ाई सप्ताहांत पर या सीमित घंटों के लिए होगी।
ऐसी बहसों के साये में एक संभावित चौंकाने वाली बात शायद कृत्रिम मेधा आधारित अलगोरिद्म की तलाश हो सकती है। दुनिया भर में शोध पर हो रही फंडिंग का करीब 80 फीसदी हिस्सा इसी क्षेत्र में जा रहा है। शुरुआती नतीजों के तौर पर कॉल सेंटरों में सभी इंसानी परिचालकों के स्थान चैटबॉट लेने लगे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगले दो से पांच वर्ष में भारत की विशालकाय कॉल सेंटर अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होगी? इसके अलावा इस दिशा में भी काम चल रहा है कि इस समय जो काम अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है उसका 90 प्रतिशत हिस्सा चैटबॉट को सौंपा जा सके। ध्यान रहे भारत के मध्य वर्ग में बड़ा हिस्सा ये काम करता है।
भविष्य में इन सबके एक साथ होने से कैसी तस्वीर बनेगी? ट्यूशन कक्षाओं की बढ़ती अर्थव्यवस्था, देश के शीर्ष पेशेवर विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए भारी प्रतिस्पर्धा, देश के निजी विश्वविद्यालयों में अनापशनाप शुल्क और कृत्रिम मेधा की बढ़ती भूमिका के जरिये विशेषज्ञ पेशेवरों को बेदखल किए जाने जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी।
आंकड़ों के खेल में कितना सच, कितना फसाना
दिलीप डिसूजा, ( कंप्यूटर विज्ञानी )
कुछ दिनों पहले हमने सुना कि भारत की अर्थव्यवस्था आकार में ब्रिटेन से बड़ी हो गई है, यानी अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद अब हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गए हैं। मगर पिछले ही दिनों एक भयानक सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, जिसने बहुत से लोगों को सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं इन दोनों खबरों के आसपास ही अपनी बात रखूंगा।
देखा जाए, तो भारत का दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय था। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा देश है, और जिस देश में जितने ज्यादा नागरिक आर्थिक रूप से सक्रिय होंगे, उसकी अर्थव्यवस्था उतनी अधिक बढ़ती जाएगी। यही वजह है कि हम उन ज्यादातर देशों से आगे निकलते जाएंगे, जहां हमारे मुकाबले बहुत कम लोग बसते हैं। ब्रिटेन की आबादी 6.72 करोड़ है, जबकि हमारी 20 गुना बड़ी करीब 1.4 अरब। हमने 75 साल में ही ब्रिटेन के साथ अपने आर्थिक फासले मिटा दिए। कमोबेश इसी तरह, हम जल्द ही जर्मनी (8.3 करोड़ आबादी) और जापान (12.6 करोड़ आबादी) को भी पछाड़ देंगे। रही बात चीन और अमेरिका की, तो जनसंख्या में चीन और हम कमोबेश बराबर हैं, और चीन व अमेरिका की अर्थव्यवस्था हमसे क्रमश: पांच व सात गुना बड़ी है, इसलिए वे लंबे समय तक हमसे आगे बने रहेंगे।हालांकि, आकार के लिहाज से अर्थव्यवस्थाओं की जब हम तुलना करते हैं, तो क्या हमें प्रति व्यक्ति आय का भी विश्लेषण नहीं करना चाहिए? आखिरकार राष्ट्र के बनिस्बत निजी आय कहीं अधिक तीव्रता से लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय 2,000 डॉलर से कुछ ज्यादा है, जबकि ब्रिटेन की 20 गुना अधिक लगभग 40,000 डॉलर। यानी, इस मामले में हम अब भी ब्रिटेन से बहुत पीछे हैं।
अब बात कार दुर्घटना की। इस हादसे ने सड़क डिजाइन, ओवरस्पीड, पिछली सीट सुरक्षा बेल्ट आदि को लेकर एक नई बहस पैदा की है। पिछली सीट पर सुरक्षा बेल्ट पहनना वाकई जरूरी है, मगर अभी कुछ अन्य तथ्यों की चर्चा। जब हम अर्थव्यवस्था के आधार पर नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के आधार पर देशों की सूची बनाते हैं, तो भारत शीर्ष की ओर बढ़ता दिखता है। ‘आवर वर्ल्ड इन डाटा’ के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में हर साल दो लाख लोग सड़क हादसे में जान गंवाते हैं। हमसे आगे चीन है, जहां सालाना ढाई लाख लोग सड़कों पर दम तोड़ते हैं। इस दौड़ में कोई अन्य देश हमारे आस-पास नहीं ठहरता। ब्राजील (45 हजार), अमेरिका (41 हजार) और इंडोनेशिया (37 हजार) शीर्ष पांच के अन्य देश हैं। अगर अर्थव्यवस्था की तरह सड़क हादसे में होने वाली प्रति व्यक्ति मौत का आंकड़ा निकालें, तो ब्राजील में प्रति 10 लाख में 211 लोग, चीन में 179, भारत में 145, इंडोनेशिया में 135 और अमेरिका में 124 लोग सड़कों पर जान गंवाते हैं। यहां शीर्ष पांच देशों में ब्राजील सबसे ऊपर और भारत तीसरे स्थान पर जरूर दिखता है, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू कुछ और कह रहा है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में सबसे ज्यादा 22 लाख सड़क हादसे हर साल होते हैं, जिसके बाद भारत में करीब पांच लाख और चीन मेें 2.12 लाख। अब इन संख्याओं को सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत से विभाजित करें, तो अमेरिका में जहां हर 50वीं दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होती है, वहीं भारत में हर दूसरी दुर्घटना में और चीन में हर हादसे में। इसी तरह, गाड़ियों की संख्या के मामले में चीन (30.7 करोड़) शीर्ष पर है, जबकि अमेरिका (29.1 करोड़) दूसरे स्थान पर और भारत (8.9 करोड़) तीसरे स्थान पर। यानी, हर दस लाख गाड़ियों पर अमेरिका में सड़क हादसे से 141 मौत होती हैं, जबकि चीन में 814 और भारत में 2,247। यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन गाड़ियों में दोपहिया वाहन शामिल नहीं हैं, जिनकी संख्या अपने देश में मोटरकारों की तुलना में करीब तीन गुना अधिक है। लिहाजा मौजूदा हालात जश्न मनाने वाले हैं या चिंता जताने वाले, यह आप खुद सोचें।
