
10-04-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date: 10-04-25
Date: 10-04-25
125% Vs 84% = Chaos
Why other countries shouldn’t think they will escape the consequences of a US-China trade war
TOI Editorials

With Trump piling on an extra 50% tariff on Chinese exports to US – taking overall tariffs on Chinese goods to 104% – Washington has started the trade version of a slap fight with Beijing. In response, China hit back and raised its own tariff on US goods to 84%. While some countries have sued for negotiations and are sending trade delegations to Washington, China has said it is ready to fight to the end.
Given this, many countries may be inclined to adopt the view that the fallout of the trade fight will only be confined to US and China. But it won’t be so easy. First, Trump is on an unpredictable path – he has now threatened to tariff the pharma industry which will impact India, even as New Delhi tries to negotiate a trade deal. Second, EU too has approved 25% tariff on US goods in another pain-point for global trade. Third, as the largest trading nation and manufacturer, China’s supply chains are like a spider-web that covers the whole world. Untangling from this will be painful no matter where you are on the Trump tariff spectrum. Case in point, for more than 15 years China’s-exports of finished consumer electronic products have exceeded all other countries combined. In 2023, China represented over 65% of laptop and tablet exports and 47% of smartphone exports by value. Additionally, China accounted for nearly a fifth of global exports of intermediate inputs like transistors, PCBs and memory chips. This means that even if an electronic product is made in a third country, chances are its components were made in China.
This perhaps explains China’s confidence in this trade war. Experts believe that Beijing has been developing a retaliatory toolbox precisely for this moment. In fact, China is so price competitive that even with 100%-plus tariff Chinese trade volumes to US could still be 30-50% of earlier numbers. But that won’t be the case for US exports to China. And if Beijing starts targeting US services – like law firms operating in China – and adopting non-tariff barriers – halting export licences for rare earths – American firms will be in serious trouble.
That, of course, will have serious consequences for US consumers and ripple effects for other countries. Add to this growing worries about dumping of Chinese products in non-US markets. Trump is right that China’s yawning trade deficit with US has been a concern for several White House administrations. But since China joined WTO in 2001, US policy has been to mould and correct China’s behaviour, not press it into a corner like Trump is trying to do. With China today far wealthier and much more powerful than it was two decades ago, potential consequences of cornering Beijing can be hugely and globally disruptive.
Date: 10-04-25
Matter Of Shame
That an upper caste neta ‘purified’ a temple visited by a Dalit neta is shocking, and as BJP knows, politically damaging
ET Editorials
The idea that untouchability may still be practised in India sounds outrageous. But the shameful fact is, instances routinely crop up of ‘purifying’ ceremonies when those beyond the caste system (varnas), Dalits, visit temples. Even so, it’s a shocking new low point that a former BJP MLA dared to ‘purify’ a temple visited by Congress Leader of Opposition in Rajasthan assembly. BJP suspended its veteran party member, a cow vigilante. Such caste prejudice may escape the law which deals with mostly direct forms of assault, insult, or obstruction that include temple entry. But such egregious ‘purification’ is no less a caste atrocity.
Point is Gyandev Ahuja and his ilk are teflon-coated. They wear their casteism as a badge of honour, proud and devout. Some elements of Hindu far-right have long argued that upper castes exerting control of temples isn’t discrimination, that it instead helps “preserve identity”. That modern India’s ‘social justice’ dharma damages caste traditions. India’s founding fathers, in their wisdom, recognised equality as the foundation for the independent nation. The likes of Gyandev Ahuja, born in independent India, have long flouted the law of the land. One of Hindu far-right’s long-standing demands is that the state exit control of temples. Ahuja’s actions, and his status as a seasoned politician, again show why state control of Hindu temples is essential, simply to ensure rule of law.
As for political fallout, BJP moved swiftly to contain the potential damage – Dalits are a key BJP base. Across the heartland, the Dalit vote has been a key part of BJP’s social engineering. How damaging a substantial loss of Dalit vote can be was clear from LS polls, when the ‘Constitution’ issue cost BJP dear in a state like UP. But this is beyond politics – it’s just shameful a senior politician would do this.
Legal milestone
Cooperative federalism must guide conduct of Governors
Editorial
The Supreme Court’s judgment on the conduct of Tamil Nadu Governor R.N. Ravi is set to have a far-reaching impact on Centre-State relations, underscoring as it does India’s federal principles in what are undoubtedly fraught times. The verdict enhances the administrative autonomy of States, and regulates the functioning of constitutional offices, with implications for the entire country. In the case which concerns Mr. Ravi’s handling of 10 Bills passed by the State Assembly, the Court has effectively changed how Governors carry out their constitutional responsibilities. The intervention comes at a time when tensions between Governors and governments in States ruled by parties other than the BJP have peaked — especially over issues such as the appointment of Vice-Chancellors (V-Cs) to State-run universities, where Governors serve as Chancellors. It is no coincidence that the Bills at the heart of the case sought to replace the Governor with the State government as the authority for appointing V-Cs. Mr. Ravi had forwarded these Bills to President Droupadi Murmu after they were re-adopted by the State Assembly. The Court held that the Bills were deemed to have received assent. It described the Governor’s action of referring the Bills to the President as “not bona fide”, and his conduct as “arbitrary, non est, and erroneous in law” — language that resembled a performance appraisal of the gubernatorial office. In normal circumstances, such a severe reprimand would have resulted in the resignation of the person whose conduct was under scrutiny: Mr. Ravi. But these are not normal circumstances, and Mr. Ravi was certainly playing the politically partisan role assigned to him by the government at the Centre, led by the BJP, which is inimically disposed to the DMK that is in power in Tamil Nadu. Hindrance was the strategy.
The significance of the judgment goes beyond the censure of a particular Governor. It lays down definite timelines for Governors to act on Bills. It ensures that Governors can no longer indefinitely delay legislation under the pretext of scrutiny or act whimsically or with impunity. The Court has reaffirmed a constitutional principle that has often been undermined: that Raj Bhavans must function with transparency, and accountability. With the legislation now in force, the Tamil Nadu government has the authority to appoint V-Cs and must act swiftly to fill these vacancies in 12 universities, and are made based on merit, integrity, and competence, given past allegations of corruption. This judgment is not merely a legal milestone; it is a call for constitutional morality and cooperative federalism, and restoration of dignity to the office of the Governor, who, as the Court pointed out, is expected to act as friend, philosopher, and guide to the State Cabinet, and not as a blunt instrument of the Centre.
सुप्रीम कोर्ट का राज्यपालों पर फैसला स्वागतयोग्य है
संपादकीय
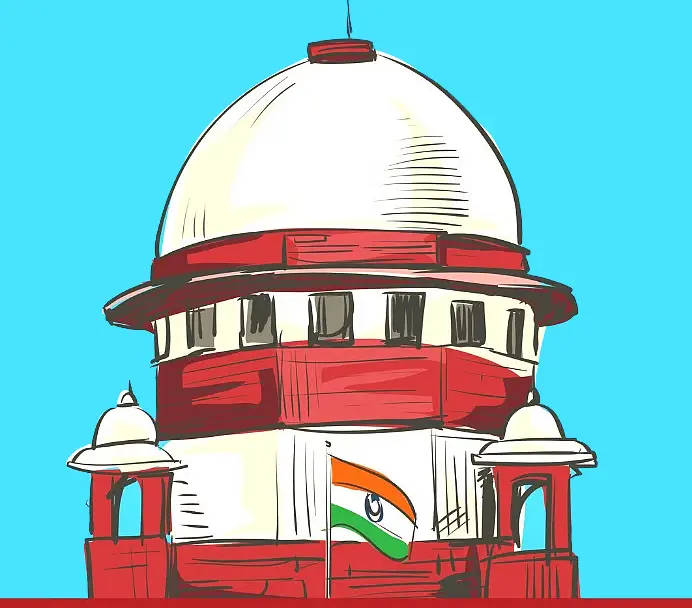
राज्यपाल की संस्था को केंद्र के अंतर्गत रखना संविधान निर्माताओं की ऊहापोह की मनःस्थिति का सबूत है। अन्य संस्थाओं से अलग मुकाम देते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन्होंने संविधान का संरक्षक तो बनाया लेकिन राज्यपाल का अस्तित्व ‘राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत’ रखा, यानी केंद्र एक अदनी-सी चिट्ठी के जरिए राज्यपाल को हटा सकता है। नतीजतन यह संस्था रीढ़विहीन होती गई। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की किसी बेंच ने अपनी असाधारण शक्तियों (अनुच्छेद 142 में प्रदत्त) का प्रयोग हुए राज्यपाल को विधायिका से पारित विधेयकों के मामलों में समयसीमा में बांधा है। हालांकि संविधान ने ‘महामहिम’ की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बिल पर हस्ताक्षर करने, उसे पुनर्विचार के लिए भेजने या राष्ट्रपति को प्रेषित करने की अवधि न स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद 200 में मात्र ‘यथासंभव शीघ्रता के साथ’ का भाव व्यक्त किया, लेकिन कालांतर में महामहिमों ने इसके दो मतलब लगाए । पहला, ठंडे बस्ते में डालना, और दूसरा, दोबारा विधायिका के भेजने पर दस्तखत करने की संवैधानिक मजबूरी की काट के लिए राष्ट्रपति को भेजना। कोर्ट ने इन दोनों को संविधान के खिलाफ माना। आज लगभग हर उस राज्य में जहां विपक्ष की सरकार है, राज्यपाल की संस्था निर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ संघर्षरत है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्पीकर की संस्था को भी सही राह पर ला सकेगा।
Date: 10-04-25
चुनौतियों का सामना
संपादकीय
अमेरिका की ओर से चीन पर 104 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले के बाद जिस तरह चीन ने भी उस पर टैरिफ दर 34 से बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दी, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि यह लड़ाई और तेज होगी और पूरी दुनिया पर उसका बुरा असर कहीं अधिक गहरा होगा।
इसकी आशंका इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी मनमानी जारी रहेगी, भले ही इससे शेष विश्व के साथ अमेरिका को भी नुकसान क्यों न हो।
ट्रंप अपनी टैरिफ नीति के दुष्परिणामों से किस तरह बेपरवाह हैं, इसका पता इससे चलता है कि देश-विदेश में तमाम विरोध के बाद भी वह अपने कदम पीछे खींचने के कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। अब जब यह स्पष्ट है कि ट्रंप विश्व व्यापार व्यवस्था का बेड़ा गर्क करने पर आमादा हैं, तब भारत को टैरिफ वार के दुष्प्रभावों से बचने के लिए कमर कस लेनी चाहिए।
इस भरोसे रहना ठीक नहीं होगा कि अमेरिका से जल्द व्यापार समझौता हो जाएगा। ऐसा कोई समझौता तभी संभव है, जब अमेरिका भारतीय हितों की भी चिंता करेगा। कहना कठिन है कि ट्रंप इसके लिए तैयार होंगे।
भारत को यह मानकर भी नहीं चलना चाहिए कि उसके प्रतिस्पर्धी देशों पर अधिक अमेरिकी टैरिफ के चलते भारतीय निर्यातकों को अपेक्षाकृत कम नुकसान होगा, क्योंकि इनमें से कुछ देश अमेरिकी उत्पादों पर अपनी टैरिफ दरें शून्य करने के संकेत दे रहे हैं।
भारत को इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि टैरिफ पर अमेरिका और चीन के बीच तीखी तकरार के चलते इसकी आशंका उभर आई है कि देश में चीनी सामान की डंपिंग हो सकती है। भारत को इसे रोकने के लिए तो जतन करने ही होंगे, भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए नए बाजार भी देखने होंगे। सरकार को निर्यातकों के साथ मिलकर वे उपाय अमल में लाने के लिए सक्रिय हो जाना चाहिए, जिनसे निर्यात में गिरावट न आने पाए।
यह समझ आता है कि भारत सरकार ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर कोई जवाबी कदम उठाने के पक्ष में नहीं, लेकिन उसे भारतीय निर्यातकों को भरोसे में लेने का काम तो करना ही चाहिए। टैरिफ वार के रूप में अमेरिका की ओर से जो चुनौती खड़ी की गई है, उसे अवसर में तभी बदला जा सकता है, जब संभावित समस्याओं का समाधान आगे बढ़कर करने की नीति पर चला जाएगा।
यह अच्छा है कि गत दिवस रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कमी कर कर्ज सस्ता करने का फैसला लिया। माना जा रहा है कि इससे घरेलू बाजार में खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसा वास्तव में हो, इसके लिए सरकार को भी अपने स्तर पर सक्रिय होना चाहिए।
 Date: 10-04-25
Date: 10-04-25
उचित नीतिगत समायोजन
संपादकीय
वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अनिश्चितता में और इजाफा नहीं करके बेहतर काम किया है। वित्तीय बाजारों की उम्मीद के मुताबिक ही बुधवार को एमपीसी ने एकमत होकर यह निर्णय लिया कि नीतिगत रीपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके उसे 6 फीसदी किया जाएगा। उसने नीतिगत रुख को भी तटस्थ से बदलकर समायोजन वाला कर दिया।
इसका अर्थ यह है कि अगर कोई आर्थिक झटका नहीं लगा तो नीतिगत रीपो दर में और इजाफा नहीं किया जाएगा। एमपीसी अपनी आगामी बैठक में केवल नीतिगत दर में कटौती करने या यथास्थिति बरकरार रखने पर विचार करेगा। हालिया अतीत में रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में बदलाव और नकदी संबंधी उपायों की बदौलत इनका असर जमीन तक पहुंचने की गति में सुधार होना चाहिए।
अमेरिका द्वारा टैरिफ में भारी इजाफा किए जाने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता तेजी से बढ़ी है लेकिन इस सप्ताह एमपीसी द्वारा लिया गया निर्णय काफी बेबाक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर में कमी आई है। मोटे तौर पर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। उम्मीद है कि यह रिजर्व बैंक के मध्यम अवधि के 4 फीसदी के लक्ष्य के आसपास ही रहेगी।
रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान को 4.2 फीसदी से कम करके 4 फीसदी कर दिया है। वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में मुद्रास्फीति की दर लक्ष्य से कम बनी रहने की उम्मीद है। व्यापारिक तनावों के कारण धीमी वैश्विक वृद्धि की आशंकाओं को देखते हुए और अमेरिका द्वारा चीन के आयात के लिए अपने रास्ते लगभग बंद कर लेने के कारण शेष विश्व में कीमतों पर नकारात्मक दबाव निर्मित होगा।
हाल के दिनों में कच्चे तेल तथा अन्य जिंसों की कीमत में भी काफी गिरावट आई है। अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात पर उच्च टैरिफ तथा व्यापक अनिश्चितता भारत की वृद्धि पर भी असर डालेगी। रिजर्व बैंक ने वर्ष के लिए अपने वृद्धि अनुमान में 20 आधार अंकों की कमी करके उसे 6.5 फीसदी कर दिया है। अनिश्चितता को देखते हुए यह मानना उचित ही है कि वृद्धि अनुमानों को संशोधित करके कम करने के आसार अधिक रहेंगे।
भविष्य में दरों संबंधी कदमों की बात करें तो अगर यह मान लिया जाए कि मुद्रास्फीति के मौजूदा पूर्वानुमान बरकरार रहेंगे तो अधिक से अधिक 25 से 50 आधार अंकों की राहत की गुंजाइश रहेगी। बहरहाल, ये सामान्य समय नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था विश्व युद्ध के बाद के अब तक के सबसे बड़े झटके से गुजर रही है और यह कहना मुश्किल है कि हालात कब तक स्थिर होंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसा रुख लेगी।
भारत की मौद्रिक नीति की बात करें तो घरेलू कीमतें जहां स्थिर रह सकती हैं वहीं मुद्रा पर दबाव से जोखिम उत्पन्न हो सकता है। हालांकि ताजा मौद्रिक नीति रिपोर्ट में पेशेवर पूर्वानुमान लगाने वालों ने जो अनुमान लगाए हैं वे दिखाते हैं कि चालू वर्ष में देश का चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का करीब एक फीसदी होगा। हालांकि वैश्विक अनिश्चितता के बीच वित्तीय चुनौतियां बरकरार रहेंगी। ऐसे में दीर्घावधि के और पोर्टफोलियो निवेशक भी शायद अनिश्चितता को देखते हुए निवेश नहीं करना चाहें।
यह भी संभव है कि अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर बढ़े क्योंकि टैरिफ में इजाफा किया गया है। ऐसे में फेडरल रिजर्व भी मौद्रिक नीति में अनुमानित राहत नहीं दे पाएगा। नीतिगत सख्ती की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए मुद्रा के मोर्चे पर हालात और जटिल हो जाएंगे। हालांकि रुपये का अवमूल्यन कुछ हद तक भारत को लाभ पहुंचाएगा और उच्च टैरिफ के नुकसान को थोड़ा कम करेगा। लब्बोलुआब यह है कि इस अनिश्चित माहौल में केंद्रीय बैंक को सावधानी बरतनी होगी। वित्तीय बाजारों के लिए भी यही अच्छा होगा कि वे वृद्धि पर संभावित दबाव के चलते दरों में अधिक कटौती पर दांव नहीं लगाएं।
बदलाव की मुद्रा
संपादकीय
भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार अनुमानों के मुताबिक रेपी दर में पच्चीस आधार अंक की कटौती कर दी है। करीब पांच वर्षों तक रेपो दर में कोई कटौती नहीं की गई। थी। फरवरी में पच्चीस आधार अंक की कटौती की गई थी यह दूसरी कटौती है। इससे बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ने और भवन, वाहन, कारोबार आदि के लिए कर्ज लेने वालों पर ब्याज का बोस कम होने का रास्ता आसान हो गया है। रिजर्व बैंक यह फैसला इसलिए कर पाया कि इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी नीचे आ गई हैं, गेहूं और दालों का अच्छा उत्पादन हुआ है खुदरा महंगाई का रुख नीचे की तरफ है। आगे भी महंगाई के नीचे रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक ने महंगाई चार फीसद पर रहने का अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक का लक्ष्य भी यही था कि महंगाई को चार फीसद के आसपास रखा जा सके। इसलिए अब उसने अपना ध्यान विकास दर पर केंद्रित कर दिया है। फिलहाल विकास दर साढ़े छह फीसद पर रहने का अनुमान है। जिस तरह अमेरिकी शुल्क नीति के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है, उसमें भारत के लिए अपना सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी हो गया है।
इस वक्त अच्छी बात है कि विनिर्माण क्षेत्र में सुधार नजर आ रहा है, जो चिंताजनक स्तर तक गोते लगा चुका था विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर होने का असर सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ता है। यह क्षेत्र इसलिए कमजोर पड़ा हुआ था कि महंगाई आम लोगों की सहनशक्ति से ऊपर चली गई थी और उन्होंने अपने दैनिक उपभोग में कटौती करनी शुरू कर दी थी। अब महंगाई घटी है, तो स्वाभाविक रूप से उपभोग का स्तर उठेगा, जिससे विनिर्माण क्षेत्र को बल मिलेगा। रेपो दर कम होने से ब्याज दरों में कमी आती है। इसका लाभ कर्ज लेने वालों को तो मिलता है, पर बचत खाते आदि में पैसा जमा कराने वालों को नुकसान होता है। हालांकि जिन लोगों के पास पूंजी अधिक है, वे लंबी अवधि की योजनाओं में जमा कर अधिक ब्याज का लाभ ले सकते हैं। सबसे अधिक राहत वाहन, भवन, कारोबार आदि के लिए कर्ज लेने वालों को महसूस होती है, पर बैंक चूंकि लंबे समय से कारोबारी शिथिलता से जूझ रहे हैं, वे रेपो दर में पच्चीस आधार की कटौती का लाभ तुरंत अपने ग्राहकों को देना शुरू कर देंगे, कहना मुश्किल है।
इस वक्त जिस तरह विश्व बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, निर्यात में और कमी आने की चिंता बढ़ गई है। पहले ही निर्यात के मामले में संतोषजनक वृद्धि नहीं हो पा रही थी, कई देशों के साथ व्यापार घाटा चिंताजनक दर से बढ़ रहा था, उसमें घरेलू बाजार को मजबूत करने पर बल देना होगा। रिजर्व बैंक का कहना है कि बाजार में अतिरिक्त पूंजी प्रवाह बढ़ाया जाएगा, इससे विनिर्माण क्षेत्र को बल मिलेगा, मगर खपत बढ़ाना फिर भी बड़ी चुनौती रहेगी। ऐसे में रेपो दर में कटौती का लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि घरेलू बाजार को मजबूत करने पर कितना जोर दिया जा रहा है। जब बेरोजगारी की दर पर काबू पाने और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के साधन विकसित नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें केवल रेपो दर में कटौती से आर्थिक बेहतरी का दावा करना मुश्किल ही बना रहेगा।
वक्फ के जरिये गैर – बराबरी दूर करने का आया वक्त
राजेश शुक्ला, ( आर्थिक विशेषज्ञ )
देश में संशोधित वक्फ कानून लागू हो चुका है। अब आगे इस कानून के उचित और तार्किक उपयोग की ओर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। भारत में बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से कई तेजी से विकसित होने की क्षमता वाले शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। ऐतिहासिक रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई ये संपत्तियां उपेक्षा, कानूनी विवादों और प्रशासनिक अस्पष्टता से ग्रस्त हैं। नये कानून में वक्फ रिकॉर्ड का कुल मिलाकर डिजिटल समायोजन, सुव्यवस्थित शासन और अधिक सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
भारत में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी हाशिये पर है। देश के सबसे व्यापक घरेलू आय सर्वेक्षणों में से एक प्राइस आइस 360 की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, जहां भारत की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 65,859 रुपये थी, वहीं मुसलमानों की औसतन 56,715 रुपये। यह राष्ट्रीय औसत से करीब 14 प्रतिशत कम है। मुस्लिम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति और भी खराब है। इनकी प्रति व्यक्ति आय 50, 179 रुपये थी, जो भारत में सभी सामाजिक-धार्मिक समूहों में सबसे कम है।
इसके विपरीत, अगड़ी हिंदू जातियों की प्रति व्यक्ति आय 82,749 रुपये थी, जो एससी/ एसटी / ओबीसी मुसलमानों की तुलना में 65 प्रतिशत अधिक है। मुसलमानों के बीच भी समूह विभाजन स्पष्ट रूप से मौजूद है। अगड़ी जाति के मुसलमान हाशिये पर रहने वाले मुस्लिम जातियों की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक आय अर्जित करते हैं। साल 2005 और 2021 के बीच, हिंदू एससी और एसटी वर्गों के प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय 637 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जबकि मुस्लिम अगड़ी जातियों में यह वृद्धि दर 625 प्रतिशत की रही है। हिंदू ओबीसी की प्रति व्यक्ति आय में 550 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यहां तक कि सबसे गरीब समूह- मुस्लिम एससी, एसटी और ओबीसी की प्रति व्यक्ति आय में भी 494 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि विकास हो रहा है, लेकिन समानता में यथोचित बदलाव नहीं हो रहा है।
मुस्लिम एससी, एसटी और ओबीसी समूह के केवल 12 प्रतिशत परिवार नौकरियों को अपनी प्राथमिक आय का स्रोत बताते हैं और केवल 14 प्रतिशत परिवारों में स्नातक स्तर के शिक्षित सदस्य हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, खासकर जब हिंदू अगड़ी जातियों से तुलना की जाती है। हिंदू अगड़ी जातियों में 31 प्रतिशत परिवार नौकरियों पर निर्भर हैं और 30 प्रतिशत परिवारों में स्नातक स्तर के शिक्षित सदस्य हैं। ऐसे में, अगर सोच-समझकर काम किया जाए, तो वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास संबंधी सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने का उपकरण बन सकता है।
संभावनाएं अपार हैं। वक्फ संपत्तियों का उपयोग उन क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, जहां मुस्लिम साक्षरता और स्नातक दर बहुत कम है । जिन क्षेत्रों में मुस्लिम युवाओं को कम कमाई होती है या कम वेतन मिलता है, उन क्षेत्रों में उन्हें व्यावसायिक रूप से शिक्षित प्रशिक्षित करना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियां किफायती आवास परियोजनाओं या छोटे उद्यमों और कारीगरों को संरक्षण देने का भी काम कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं और युवाओं को सवाल पूछना चाहिए कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग कैसे किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर आम लोगों की भागीदारी के बिना, इस पर अभिजात वर्ग के कब्जे या राजनीतिक दुरुपयोग का जोखिम बना रहेगा।
भारत का भविष्य न केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ती है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसके विकास के लाभ का वितरण कितनी निष्पक्षता से कितने लोगों के बीच हो रहा है। जैसे-जैसे हम पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, न्याय और समता को केवल सांविधानिक आदर्शों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो वक्फ कानून हमें दिशा दिखा सकता है।
देश में संशोधित वक्फ कानून लागू हो चुका है। अब आगे इस कानून के उचित और तार्किक उपयोग की ओर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। भारत में बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से कई तेजी से विकसित होने की क्षमता वाले शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। ऐतिहासिक रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई ये संपत्तियां उपेक्षा, कानूनी विवादों और प्रशासनिक अस्पष्टता से ग्रस्त हैं। नये कानून में वक्फ रिकॉर्ड का कुल मिलाकर डिजिटल समायोजन, सुव्यवस्थित शासन और अधिक सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
भारत में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी हाशिये पर है। देश के सबसे व्यापक घरेलू आय सर्वेक्षणों में से एक प्राइस आइस 360 की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, जहां भारत की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 65,859 रुपये थी, वहीं मुसलमानों की औसतन 56,715 रुपये। यह राष्ट्रीय औसत से करीब 14 प्रतिशत कम है। मुस्लिम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति और भी खराब है। इनकी प्रति व्यक्ति आय 50, 179 रुपये थी, जो भारत में सभी सामाजिक-धार्मिक समूहों में सबसे कम है।
इसके विपरीत, अगड़ी हिंदू जातियों की प्रति व्यक्ति आय 82,749 रुपये थी, जो एससी/ एसटी / ओबीसी मुसलमानों की तुलना में 65 प्रतिशत अधिक है। मुसलमानों के बीच भी समूह विभाजन स्पष्ट रूप से मौजूद है। अगड़ी जाति के मुसलमान हाशिये पर रहने वाले मुस्लिम जातियों की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक आय अर्जित करते हैं। साल 2005 और 2021 के बीच, हिंदू एससी और एसटी वर्गों के प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय 637 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जबकि मुस्लिम अगड़ी जातियों में यह वृद्धि दर 625 प्रतिशत की रही है। हिंदू ओबीसी की प्रति व्यक्ति आय में 550 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यहां तक कि सबसे गरीब समूह- मुस्लिम एससी, एसटी और ओबीसी की प्रति व्यक्ति आय में भी 494 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि विकास हो रहा है, लेकिन समानता में यथोचित बदलाव नहीं हो रहा है।
मुस्लिम एससी, एसटी और ओबीसी समूह के केवल 12 प्रतिशत परिवार नौकरियों को अपनी प्राथमिक आय का स्रोत बताते हैं और केवल 14 प्रतिशत परिवारों में स्नातक स्तर के शिक्षित सदस्य हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, खासकर जब हिंदू अगड़ी जातियों से तुलना की जाती है। हिंदू अगड़ी जातियों में 31 प्रतिशत परिवार नौकरियों पर निर्भर हैं और 30 प्रतिशत परिवारों में स्नातक स्तर के शिक्षित सदस्य हैं। ऐसे में, अगर सोच-समझकर काम किया जाए, तो वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास संबंधी सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने का उपकरण बन सकता है।
संभावनाएं अपार हैं। वक्फ संपत्तियों का उपयोग उन क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, जहां मुस्लिम साक्षरता और स्नातक दर बहुत कम है । जिन क्षेत्रों में मुस्लिम युवाओं को कम कमाई होती है या कम वेतन मिलता है, उन क्षेत्रों में उन्हें व्यावसायिक रूप से शिक्षित प्रशिक्षित करना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियां किफायती आवास परियोजनाओं या छोटे उद्यमों और कारीगरों को संरक्षण देने का भी काम कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं और युवाओं को सवाल पूछना चाहिए कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग कैसे किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर आम लोगों की भागीदारी के बिना, इस पर अभिजात वर्ग के कब्जे या राजनीतिक दुरुपयोग का जोखिम बना रहेगा।
भारत का भविष्य न केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ती है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसके विकास के लाभ का वितरण कितनी निष्पक्षता से कितने लोगों के बीच हो रहा है। जैसे-जैसे हम पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, न्याय और समता को केवल सांविधानिक आदर्शों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो वक्फ कानून हमें दिशा दिखा सकता है।