
07-02-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:07-02-23
Date:07-02-23
Municipal Mess
From MCD to BMC, paralysis of urban local bodies undermines local governance and democracy
TOI Editorials
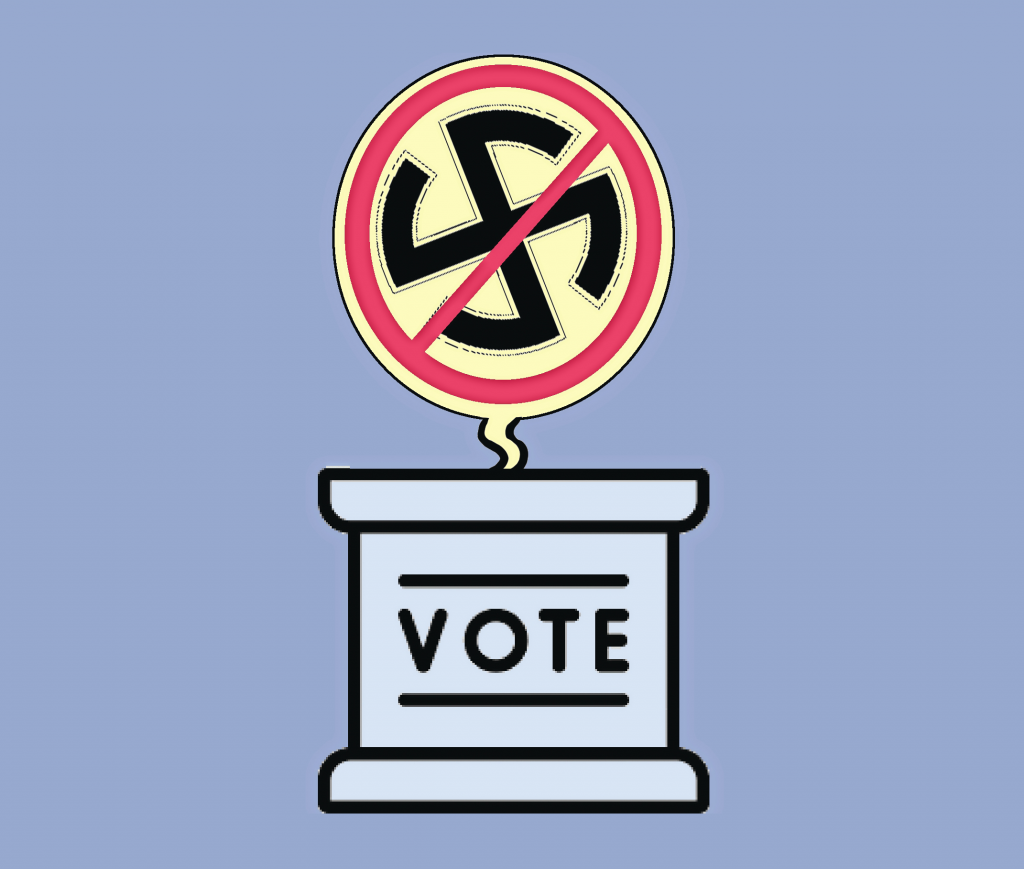
True, in the absence of a mayor – as well as deputy mayor and standing committee – a special officer is in charge. But major decisions related to policy matters, development works and projects that require big financial investment are delayed. Surprisingly, MCD isn’t the only municipal body in this position. For close to a year, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) – the country’s richest civic body – has been managed by an administrator after its term expired and polls were delayed. Further, an astonishing 22 of 28 municipal corporations in Maharashtra have seen their terms expire with fresh polls nowhere in sight.
Such atrophy also undermines local democracy. The Constitution (74th Amendment) Act, 1992 provided for the creation of urban local bodies and empowered state governments to devolve the responsibility of 18 functions including urban planning, regulation of land use, water supply etc. But a 2020 paper by PRS Legislative Research found that most state governments are reluctant to share power and taxes with local bodies. This severely curtails urban governance at a time when 675 million Indians are slated to live in urban centres by 2035. They need smarter cities, which needs empowered instead of stalled local bodies. Mumbai needs municipal elections. Delhi needs a mayor.
What India Needs is A Greendustrial Plan
ET Editorials
Inaugurating the India Energy Week 2023, the first major event in the G20 calendar, the PM highlighted the immense growth opportunities across India’s energy landscape. Though it addresses individual behaviour and consumption choices, the Lifestyle for Environment (LiFE) initiative is replete with opportunities to leverage sustainable and low-emission options. What India needs, and is missing, is a strategic green industrial plan.
India’s clean energy transition has been largely focused on domestic market formation to make the most of the decline in renewable energy (RE) costs. The aim of cost-effectiveness and minimisation has meant little attention to clean energy R&D. Long-term technology upgrading did not fit the needs. Consequently, investment in R&D and its deployment has been minuscule. The production-linked incentives (PLI) to promote RE equipment manufacturing and the green hydrogen and energy storage missions offer something of a course correction. But they are not enough.
The world’s leading economies have rolled out green industrial plans with protectionist hues — the Inflation Reduction Act in the US, and the Green Industrial Strategy in China. A green subsidies war is brewing and barriers to export of relevant technologies are being erected. This situation will impact clean technology investments and trade, leaving emerging economies like India at a disadvantage. Safeguarding India’s decarbonisation and economic growth requires a green industrial strategy focused on investing in creating local capacities for innovation, R&D and deployment of technologies. It must create partnerships among industry, public and private sectors, and academia, leading to investment across multiple clean-technology value chains.
End-of-life decisions
SC’s tweaks on directive norms are welcome, but legislation will be better
Editorial
When the Supreme Court granted legal status to the concept of ‘advance medical directives’ in 2018 and allowed passive euthanasia, subject to stringent safeguards, it was seen as a vital recognition of both patient autonomy over end-of-life decisions and the right to a dignified death. However, doctors later found that some of the specific directions turned out to be “insurmountable obstacles”. In a recent order, a Constitution Bench modified the directions to make them more workable and simple. The advance directive no more needs to be countersigned by a judicial magistrate. Instead, it could be attested before a notary or a gazetted officer. Instead of the magistrate, it is enough if the notary or officer is satisfied that the document is executed voluntarily, without coercion or inducement, and with full understanding. The original guideline that the executor should name a guardian or a close relative who would be authorised to give consent to refuse or withdraw medical treatment, in the event of the executor becoming incapable of a decision, has been modified to name more than one guardian or relative. Instead of the magistrate being tasked with informing family members about the document, in case they are not present at the time of its being executed, the onus is now on the persons themselves to hand over a copy of the advance directive to the guardians or close relatives named in it, as well as to the family physician. It may also be included in digital health records.
The new guidelines require the hospital itself to constitute a primary medical board to certify whether the instructions on refusal or withdrawal of treatment should be carried out. The hospital should also form a secondary board, including a doctor nominated by the district’s chief medical officer, which will have to endorse the primary board’s certificate. The change here is that the district Collector need not constitute the second medical board, as required in the 2018 judgment. The scrutiny by the boards holds good even in cases in which there is no advance directive, but the patient is not in a position to make any decision. The new guidelines also spell out the experience and specialisations of those to be included in the medical boards. While such guidelines are useful and necessary to implement the concept of a ‘living will’ and advance medical directives, it is time Parliament came out with a comprehensive law. Such a law could also provide for a repository of advance directives so that the need to ascertain afresh its genuine nature does not arise at the time of its implementation.
संघ प्रमुख के बयान पर अमल करे समाज
संपादकीय
आरएसएस प्रमुख ने संत रविदास जयंती पर तीन बेहद गंभीर बातें कहीं हैं। पहली, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है; दूसरी, शिवाजी द्वारा औरंगजेब को लिखे पत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दू-मुसलमान सब ईश्वर के बनाए हैं लिहाजा उनमें फर्क न करें; और तीसरी, कोई भी समाज 30% से ज्यादा नौकरियां नहीं दे सकता लिहाजा लोगों को स्व-रोजगार की ओर जाना होगा। दुनिया के सबसे बड़े वैचारिक संगठन के मुखिया का यह बयान केवल हिन्दुओं ही नहीं सभी धर्मों के अनुयाइयों के लिए ध्रुवतारा बन सकता है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर पिछले कुछ दिनों से कुछ नेता मानस को जातिवाद का पोषक और ऊंच-नीच को हवा देने वाला बता रहे हैं। इसके कारण जातिवादी दुराव बढ़ रहा है। जब उच्च जाति का कोई व्यक्ति, किसी दलित वर्ग के दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोकता है या एक धर्म के लोग किसी अन्य धर्म के व्यक्ति पर कुछ भी थोपते हैं, तो शायद उन्हें ईश्वरीय व्यवस्था की समझ नहीं होती। इस ओर संघ प्रमुख ने विगत दशहरे पर इंगित किया था। आज यही बात उन आतंकियों को भी सोचनी होगी, जिन्हें लगता है कि वे हत्याएं करके ऊपरवाले का हुक्म मान रहे हैं। समाज में ये दोनों सोच इसे सदियों पीछे धकेल रही हैं। संघ प्रमुख का कहना कि नौकरियों के पीछे भागने की जगह स्व-उद्यम लगाएं, यह एक अच्छी सलाह है। लेकिन लगातार बदलते तकनीकी और पूंजी के प्रभुत्व के दौर में स्व-रोजगार की सीमा मात्र पकौड़े बेचने तक सीमित हो जाती है। इसके उलट सरकारी या संगठित क्षेत्र की नौकरी उन्हें भविष्य की सुरक्षा देती है।
 Date:07-02-23
Date:07-02-23
शीर्ष न्यायालय की सर्वोच्चता और उससे जुड़े कुछ सवाल
जैमिनी भगवती

तकरीबन आधी सदी पहले अप्रैल 1976 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के कुख्यात मामले में अपनी न्याय की समझ को तत्कालीन केंद्र सरकार के सामने समर्पित कर दिया था। देश के मुख्य न्यायाधीश ने 1975-77 के दौरान सरकार के कहने पर उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर दिया था जो मुश्किल हालात पैदा कर रहे थे। 1970 के दशक के मध्य से ही भारत की सरकारें अक्सर प्रयास करती रही हैं कि उच्च न्यायालयों में अथवा सर्वोच्च न्यायालय में उनकी पसंद के न्यायाधीश चुने जाएं। न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया आयोग ने 2002 में अनुशंसा की थी कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए जिसमें मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुशंसित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हो। आयोग ने अनुशंसा की थी कि प्रस्तावित एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करे।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अपनी संपत्ति का खुलासा करना जरूरी नहीं है जबकि सरकारी अधिकारियों तथा चुनाव लड़ने वालों के लिए ऐसा करना जरूरी है। अक्सर न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद पंचाट के सदस्य, राज्य सभा के सदस्य और राज्यपाल तक बन जाते हैं। कुछ मामलों में तो सेवारत न्यायाधीशों ने सार्वजनिक तौर पर सत्ता पक्ष के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की और सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद उन्हें सरकार द्वारा महत्तवपूर्ण पदों पर बिठा दिया गया। फिर भी आम भारतीयों को उम्मीद है कि कुछ कमियों के बाद भी एक संस्थान के रूप में सर्वोच्च न्यायालय सरकार की अतियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा।
संविधान के अनुच्छेद 348(1) में कहा गया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश भी आते हैं जिन्हें अंग्रेजी का बहुत सीमित ज्ञान होता है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने 1 अगस्त, 2022 को एक आदेश में कहा था, ‘हिमाचल उच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह समझ से बाहर है।’ यहां संदर्भ हिमाचल प्रदेश बनाम हिमाचल एल्युमीनियम ऐंड कंडक्टर्स मामले का है।
लिखने के बुनियादी कौशल और समग्र शिक्षा को लेकर एक बचाव आवश्यक है ताकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित किसी संस्था द्वारा कराई जाने वाली प्रतिस्पर्धी परीक्षा संपन्न कराई जा सके। यह एक अलग और विशिष्ट परीक्षा होनी चाहिए जहां से सभी न्यायाधीशों का चयन हो सके। कुछ महीने पहले मैंने सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से पूछा कि क्या ऐसी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिये न्यायाधीशों को चुनना व्यावहारिक और वांछित है तो उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा कि ऐसा करना आवश्यक हो चुका है।
इस समय देश की निचली अदालतों में करीब चार करोड़ मामले लंबित हैं। उच्च न्यायालयों के समक्ष 56 लाख और सर्वोच्च न्यायालय में 70,000 मामलों की सुनवाई चल रही है। अक्सर न्यायाधीश ही मामलों के स्थगन और अपील के दशकों तक खिंचने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए क्योंकि कई अदालती मामलों में वे भी शामिल होती हैं। इतने अधिक लंबित मामलों को देखते हुए क्या सर्वोच्च न्यायालय को खुद को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उपासना स्थलों या नोटबंदी जैसे मामलों से जोड़ना चाहिए? ऐसे मामले निचली अदालतों में निपट सकते हैं। शीर्ष न्यायालय को अभी चुनावी बॉन्ड के जरिये राजनीतिक दलों को गुप्त चंदे से संबंधित मामले को भी निपटाना है।
सरकार के पक्ष में काम करने की बात करें तो कुछ और ऐसे क्षेत्र हैं जहां नियंत्रण एवं संतुलन काम नहीं आया है। उदाहरण के लिए राज्यों के राज्यपाल, चुनाव आयुक्त तथा पुलिस आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक आदि पदों पर होने वाली नियुक्तियां अक्सर सत्ताधारी दलों के समर्थन के आधार होती रही हैं। यह देश की चुनाव प्रक्रिया और हमारे मतदाता वर्ग की दृष्टि से दुखद है हमें ऐसी सरकारें मिलती हैं जिन पर हम यह विश्वास नहीं कर सकते कि वे अहम पदों पर निष्पक्ष और सक्षम लोगों का चुनाव करेंगी। न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया में सरकार के नामित लोगों को शामिल करने का प्रस्ताव हमारी न्यायपालिका की निष्पक्षता और शुचिता के लिए सही नहीं होगा।
जाहिर है हमें ऐसे न्यायाधीश चाहिए जो भ्रष्ट न हों। सभी न्यायाधीशों को सेवाकाल में अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए और सेवानिवृत्ति के बाद भी 10 वर्षों तक सालाना ऐसा करना चाहिए। सक्षम न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय एक सात सदस्यीय समिति बना सकता है जिसमें मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा दो गैर सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हों। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की प्रक्रिया बिंदुवार ढंग से सामने रखी जानी चाहिए और यह सूचना सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसी समिति में कोई सरकार द्वारा नामित कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सहमति से नियुक्तियों को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में इस समिति के किन्हीं दो सदस्यों को वीटो अधिकार होना चाहिए ताकि वे किसी संभावित नियुक्ति को रोक सकें। इसके साथ ही सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वह चयन समिति द्वारा तय नामों को खारिज कर सके। बहरहाल, सरकार को इसके साथ ही विस्तार से यह भी बताना चाहिए कि वह किसी नाम को क्यों खारिज कर रही है। इस जानकारी को सदन पटल पर रखा जाना चाहिए।
विवाह की उम्र और कानून
बिभा त्रिपाठी
एक तरफ यौन स्वातंत्र्य को निजता का अधिकार माना जाता है, तो दूसरी तरफ उम्र के आधार पर अंतरराष्ट्रीय मानकों से अलग हट कर कानून बनाए जाते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि सहमति से संबंध, विवाह की उम्र और पक्षकारों के वैयक्तिक अधिकारों के विवाद पर गहन विमर्श और यथासंभव विवादित मुद्दों के निस्तारण का प्रयास किया जाए। भारतीय दंड संहिता में सहमति की उम्र, बलात्संग के प्रावधान, बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण, बाल विवाह निरोधक कानून और वैयक्तिक विधियों की स्थिति प्रमुख हो जाती है।
फिलहाल, लड़कियों के विवाह की उम्र अट्ठारह वर्ष से बढ़ा कर इक्कीस वर्ष करने का विधेयक प्रस्तावित है। किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम में बलात्संग जैसे अपराधों में लिप्त सोलह से अठारह वर्ष के बच्चों की मानसिक परिपक्वता का निर्धारण करने और तदनुसार उनके साथ दंड विधान का प्रयोग करने की बात कही गई है। न्यायपालिका द्वारा समय-समय पर ऐसे निर्णय दिए जाते रहे हैं, जो कभी अत्यधिक प्रगतिशील माने जाते हैं, तो कभी रूढ़िवादी मानसिकता के पोषक। एक तरफ विवाह के अधिकार को व्यक्ति का मौलिक अधिकार बताया गया है, तो दूसरी तरफ उम्र के विवादित होने पर कानूनी निपटारे का प्रावधान भी किया गया है। विवाह जैसी संस्था, चाहे इसे हिंदू विधि के तहत संस्कार माना जा रहा हो, चाहे मुसलिम विधि के तहत संविदा, इसकी चूलें हिल रही हैं और वयस्कों के बीच सहजीवन सामान्य जीवन शैली होती जा रही है।
ऐसे में महज उम्र का मापदंड अपराध निर्धारण के लिए संपूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता। न्यायालय में जब भी उम्र के निर्धारण का प्रश्न उठा है, इस बात की पुरजोर वकालत की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उम्र के आधार पर कानूनों के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। मगर विवाद की किसी भी स्थित में अमूमन दो वर्ष का लाभ पक्षकार बच्चे को मिलता है।
ऐसे में जब हम ‘इंडिपेंडेंट थाट बनाम भारत संघ’ के मामले में 2017 में न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर द्वारा दिए निर्णय को देखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे सामने आया प्रश्न काफी सार्वजनिक महत्त्व का है कि क्या एक पुरुष और उसकी पत्नी के बीच- पंद्रह से अठारह साल की उम्र की लड़की होने के संबंध में- यौन संबंध बलात्कार है? भारतीय दंड संहिता में इसका उत्तर नकारात्मक है, मगर हमारी राय में अठारह साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बलात्कार है, चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं। ऐसा लगता है कि तभी से वैवाहिक बलात्संग का प्रश्न अपने उत्तर तलाश रहा है।
दूसरी तरफ बाल विवाह निरोधक कानून अठारह वर्ष से कम उम्र के विवाह को शून्य घोषित करता है, पर ऐसे विवाह से भी अगर कोई संतान उत्पन्न हो जाती है, तो फैक्टम वैलेट के सिद्धांत के तहत ऐसी संतान को जायज मानते हुए उसे समस्त अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले को देखें, जहां एक सत्रह वर्ष की अवयस्क मुसलिम लड़की ने प्रेम में पड़ कर मुसलिम विधि के अनुसार विवाह किया, पर अपने माता-पिता द्वारा प्रताड़ित की जा रही थी। उसने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई, तब न्यायालय ने न सिर्फ उसे सुरक्षा प्रदान करने की अनुशंसा की, बल्कि यह भी कहा कि वह चाहे तो अपने पति के साथ रह सकती है। पर न्यायालय ने यह भी कहा कि इस आधार पर आगे के मामले निर्णीत न किए जाएं।
उधर इस निर्णय के दो ही महीने बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने नाबालिग मुसलिम लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक नाबालिग मुसलिम लड़की का यौवन या पंद्रह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर विवाह, बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन नहीं करेगा। पीठ ने आगे कहा कि पाक्सो अधिनियम, एक विशेष अधिनियम होने के नाते, पर्सनल ला को दरकिनार करता है।
इस प्रकार के निर्णयों में विभिन्न उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोणों में भिन्नता की वजह से अब सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने संसद से अपील की है कि पाक्सो अधिनियम में सहमति की निर्धारित उम्र को अठारह वर्ष से कम करने पर विचार करे। इस अपील के पीछे मंशा यही रही होगी कि ऐसे किशोर वय के बच्चे अगर प्रेम में पड़कर आपसी सहमति से संबंध बनाएं तो उन्हें अपराधी न समझा जाए। मगर सरकार ने इस पर सहमति नहीं जताई है।
स्पष्ट है कि निश्चित ही ये मामले बेहद संवेदनशील हैं। कहीं मानसिक परिपक्वता के अभाव में, तथाकथित उदासीनता के शिकार युवा परिवार और समाज के प्रति विरोध का स्वर मजबूत करते हुए ऐसे संबंध बनाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि किशोरावस्था में लिया गया निर्णय गलत साबित हो गया है, तो कहीं माता-पिता स्वयं अपने बच्चों के बाल विवाह के दोषी पाए जाते हैं। कहीं समाज द्वारा पक्षकारों पर इसलिए अत्याचार किया जाता है कि उन्होंने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर ऐसे संबंध स्थापित किए हैं। ऐसे में समस्या का निस्तारण किस प्रकार किया जाए यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है।
फिलहाल दो मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। पहला, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग द्वारा लड़कियों के विवाह की उम्र को अठारह वर्ष से बढ़ा कर इक्कीस वर्ष किए जाने की और दूसरे सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा सहमति से संबंध की उम्र को अठारह से घटा कर सोलह वर्ष किए जाने की। अब सोचना यह है कि अगर संसद विवाह की उम्र को बढ़ाकर इक्कीस वर्ष भी कर देती है तो इसका प्रभाव उसी पर होगा, जो विवाह जैसी संस्था पर भरोसा करता है। बिना विवाह के आपसी सहमति से साथ रहने वालों की स्थिति तब भी नाजुक ही रहेगी। और अगर उम्र घटा कर सोलह वर्ष कर दी गई, तो अनेक प्रकार की समस्याएं सामने आएंगी। कभी उनके अपने माता-पिता और परिवार द्वारा ही मुकदमा दायर होगा, तो कभी पक्षकारों में से ही किसी द्वारा विवाह के झांसे में संबंध बनाने का मामला आएगा और न्यायालय को सहमति की स्वतंत्रता के प्रश्न पर मगजमारी करनी होगी। सबसे गंभीर समय तब आएगा जब पक्षकारों में से कोई अन्य धर्म का होगा।
इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कैसे विवाह जैसी संस्था को बचाया जाए और परिवार तथा समाज अपने बच्चों का समाजीकरण स्वस्थ ढंग से करते हुए संवादहीनता की स्थिति को हर हाल में समाप्त कर पाए। हमारे आपराधिक न्याय प्रशासन में अब भी पीड़ित की हित रक्षा का मुद्दा हाशिये पर ही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहां अपराधों की संख्या में कमी आ रही है, अपराधियों के सुधार और पुनर्वास पर घोषणापत्र तैयार हो रहे हैं और पीड़ित को पुनर्स्थापित करने के लिए नई-नई नीतियां बनाई जा रही हैं, वहां इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ना ही होगा कि भारतीय समाज अपनी पितृसत्तात्मक सोच के साथ कब तक चलेगा? इसलिए समय की मांग है कि हम प्रेम, दबाव, शोषण और भयादोहन जैसे शब्दों में अंतर की बारीकी को समझें और हर मामले का निस्तारण उसके विशेष तथ्यों के आधार पर करें।
हर हाल में संसद, समाज और न्यायपालिका को प्रगतिशील बनना होगा। इस क्रम में एक वैध विवाह की उम्र को अठारह से बढ़ाकर इक्कीस कर देना तो उचित प्रतीत होता है, पर सहमति से सबंध की उम्र घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर आने वाले समय में इसे और भी नीचे ले जाने की मांग की जा सकती है।
भारतीय परिवेश में जरूरी है
कमलेश जैन
भारत में हिंदू स्त्रियों की स्थिति 200 वर्ष पहले दयनीय थी। पंडिता रमाबाई ने कहा था भारत तब तक तरक्की नहीं कर सकता और संसार के देशों में कोई स्थान नहीं बना सकता जब तक कि हिंदू घरों में हिंदू स्त्रियां जो मां भी है, की स्थितियां नहीं सुधरती। बच्चियों को बालपन में शादी कर उपेक्षा के अंधकार में ढकेल दिया जाता है।
इसके साथ ही अपने मातृ कर्तव्यों के बारे में अनजान, खासकर सामान्य पोषण संबंधी नियमों से अनजान और ज्यादा निम्नस्तर को प्राप्त होती हैं। यह याद रखना होगा कि वह भी एक लड़की है तथा बच्चे को जन्म देकर मां बनती है। 14-15 की उम्र में उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने बच्चों का सही ढंग से पालन कर सकेगी। हम देख रहे हैं कि हिंदू रीति-रिवाजों एवं कानून में निरंतर सुधार हुआ है। सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध हुआ है। कानून में भी आवश्यक बदलाव कर लड़कियों को जकड़नों, बंधनों से मुक्त किया गया है। आज उनके विवाह की उम्र क्रमश: बढ़ाकर 18-21 वर्ष की गई है, मुफ्त शिक्षा का उपहार दिया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बदलाव लाया गया और लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष लड़कों के विवाह उम्र 21 वर्ष की गई और भी बहुत से बदलाव विवाह एवं तलाक के कानूनों में किए गए। इस कारण, आज उनकी स्थिति, शक्ति, आत्मसम्मान में काफी परिवर्तन हुआ है। ठीक इसी तरह मुस्लिम कानून में, स्त्रियों के लिहाज से परिवर्तन आज की मांग है। 1990 के दशक में भी इसकी जरूरत समझी जा रही थी। मैंने खुद ‘एप्वा’ सीपीएमएल की महिला विंग की कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रश्नावली, बनाकर पटना का भ्रमण किया था। मैंने बल्ब बनाने वाली महिला से लेकर डॉक्टर तक का इंटरव्यू लिया। सवाल थे- क्या उन्हें पढ़ना, बाहर काम करना पसंद है, क्या वे पति की अकेली पत्नी बनकर रहना चाहती हैं, क्या उन्हें तीन तलाक की प्रक्रिया पसंद है, क्या उन्हें संपत्ति में अधिकार पसंद है, क्या तलाक के बाद मुआवजा या भरण-पोषण का अधिकार चाहिए आदि। करीब-करीब सभी ने यही कहा- हां पसंद है पर मजहब की पाबंदियों के कारण कुछ कह नहीं सकती। आज इन बहनों को भी इन जकड़नों से निकलते की जरूरत है। शादी की उम्र अभी महज 15 वर्ष है। इतनी सी उम्र में शिक्षा मुश्किल से 10 क्लास हो सकती है और नौकरी कर अपने पांवों पर खड़े होने का सवाल ही नहीं उठता। यहां विवाह एक कांट्रेक्ट की तरह है जिसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। पर यहां भी पुरुष को अधिक अधिकार दिए गए हैं। मुहम्डन कानून की धारा 251 (2) के अनुसार पागलों और नाबालिगों (लड़का-लड़की) का विवाह उनके अभिभावक द्वारा 15 वर्ष से कम में भी हो सकता है। इसी कानून के अनुसार एक मुस्लिम लड़के का विवाह तोड़ा जा सकता है यदि उसकी सहमति विवाह पर नहीं है। इसके अलावा तलाक के नियम भी पुरुषों के अलग और स्त्रियों के अलग हैं। उन्हें तलाक के बाद मासिक भत्ता देने का रिवाज नहीं है। यह सिर्फ इद्दत भर है यानी तलाक देने से तीन महीनों तक। इसके अलावा स्त्री एक शादी कर सकती है जो कि ठीक है। पर पुरुष एक ही समय में 4 विवाह कर सकता है, और एक ही घर में रख सकता है और यदि वह पांचवां विवाह भी कर लेता है तो यह गैर कानूनी या गैर धार्मिक नहीं है, बस अनियमित है। ऐसी व्यवस्था में हर एक स्त्री को पति पर एकाधिकार नहीं होता जो उसे खुशी प्रदान कर सके। इसके अलावा शिया कानून में दो तरह के विवाह होते हैं- परमानेंट और मुता विवाह यानि अस्थाई। एक शिया मुस्लिम, किसी भी धर्म की स्त्री यथा मुस्लिम, ईसाई, यहूदी या पारसी के साथ अस्थाई विवाह कर सकता है, पर किसी और धर्म वाली के साथ नहीं। पर एक शिया स्त्री किसी गैर मुस्लिम के साथ मुता निकाह नहीं कर सकती। इसमें शारीरिक संबंध एक तय अवधि के लिए बनाया जा सकता है। यह अवधि एक दिन, एक महीना, एक वर्ष या डावर यानी मुआवजा देना जरूरी है। इसमें यौन संबंध की अवधि तथा ‘डावर’ दोनों ही तय होने चाहिए। स्त्री पुरुष में यह भेदभाव स्त्रियों की खुशी उन्नति, शारीरिक सुरक्षा, समाज, देश में उसकी भागीदारी को आहत करती है। इसी प्रकार भारत में हर धर्म, संप्रदाय में यथा ईसाई, पारसी, हिंदू, आदिवासी सभी में स्त्रियों के अधिकार की दृष्टि से एक ही नागरिक संहिता होनी चाहिए। देश की आधी जनसंख्या यदि संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित रहे तो उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक संपदा, लाभ से राष्ट्र वंचित रहता है। ऐसा देश दुनिया के प्रगतिशील देशों की दौड़-विकास की तुलना में पीछे हो जाता है।
इसका असर राजनीतिक तो है ही सामाजिक भी है। जिस दिन महिलाएं अपनी सशक्त उपस्थिति देश की संसद, विधानसभा, पंचायत, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, व्यापार में बराबरी से दर्ज कराएंगी तो देश अत्यंत ही सशक्त संतुलित और अहिंसक होगा। सामाजिक तौर पर शिक्षित, बालिग स्त्रियां आर्थिक रूप से मजबूत, बच्चों के पालन में संतुलित, जागृत होगी। कहा भी जाता है एक शिक्षित मां कई बच्चों की एक मजबूत आधारशिला होती है जिसके बच्चे परिपक्व और समझदार होते हैं। देश राजनैतिक परिवेश और घर समाज की समुचित उन्नति के लिए समान नागरिक संहिता अत्यंत ही आवश्यक है।
कमियों पर वक्त रहते कसे शिकंजा
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद पिछले एक सप्ताह में अडानी समूह की कंपनियों की परिसंपत्तियों में सौ खरब डॉलर से अधिक की कमी आ चुकी है और विश्व का तीसरा सबसे अमीर आदमी शीर्ष बीस की सूची से भी बाहर हो गया है। गनीमत है कि भारतीय बाजार या वित्तीय संस्थाओं में अभी तक कोई बहुत अधिक घबराहट नहीं दिखी है, पर यह सवाल तो उठना स्वाभाविक ही है कि वर्षों से चल रही अस्वाभाविक वित्तीय हरकतों पर नजर रखने वाली हमारी नियामक संस्थाएं आखिर क्या कर रही थीं?
यह पहली बार नहीं है कि देश की नियामक संस्थाएं तब तक गाफिल रहीं, जब तक कि किसी बाहरी संस्था ने कोई बड़ा भंडाफोड़ न कर दिया या घपलेबाज व्यक्ति या कंपनी किसी बैंक का ऋण चुकाने में असफल न हो गई हो। ऐसा भी नहीं है कि घपलों की आग के पीछे धुआं बिल्कुल अदृश्य रहा हो। मगर सिर्फ वे ही इसे लेकर गफलत में रह सकते हैं, जो इसे देखना ही नहीं चाहते, और वे हमारी नियामक संस्थाएं ही हैं।
रिजर्व बैंक, सेबी, ट्राई, डीआरआई, सीबीआई, एनआईए से लगायत विभिन्न राज्यों के विजिलेंस और भ्रष्टाचार निरोधक संगठन कुछ ऐसी ही नियामक संस्थाएं हैं, जिन्हें वित्तीय घपलों से निपटने के लिए बनाया गया है। यदि हम परिप्रेक्ष्य को थोड़ा विस्तृत कर देखें, तो न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों और ट्रिब्यूनल भी नियामक की तरह ही काम कर सकते हैं। पर हर्षद मेहता, केतन पारिख, विजय माल्या, नीरव मोदी या हाल के आईसीसीआई बैंक के मामलों में इन संस्थाओं में हरकत क्यों नहीं हुई या ऐसा कैसे हुआ कि सेबी जैसी एक रेगुलेटरी बॉडी में ही वर्षों तक घपला चलता रहा? ये कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न हैं, जो अडानी समूह की कंपनियों के शेयर बाजार में औंधे मुंह गिर पड़ने के बाद एक बार फिर उठ खड़े हुए हैं।
यदि हम ध्यान से देखें, तो पाएंगे कि नियामक संस्थाओं के साथ दो तरह की दिक्कतें उनके जन्म से ही जुड़ी होती हैं। किन्हीं राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय दबावों के चलते उनका गठन तो हो जाता है, लेकिन उनके अधिकारों या कर्तव्यों के क्षेत्र में ऐसे छिद्र छोड़ दिए जाते हैं, जिनका लाभ उठाते हुए कोई भी ताकतवर दोषी वर्षों तक अदालतों में दांव-पेच खेलकर अपने को बचाए रख सकता है। एक बार किसी संस्था का गठन हो जाने के बाद उसमें नियुक्त होने वाले अध्यक्ष या सदस्यों के पदों पर कई बार ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जाती है, जो सर्वथा अक्षम होते हैं या जिनकी स्वयं की निष्ठा संदिग्ध होती है। ऐसे सदस्यों वाले संगठन भ्रष्टाचार से किस हद तक लड़ सकेंगे, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। पिछले दिनों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी चित्रा रामकृष्णन का मसला बिल्कुल बाड़ द्वारा खेत खाने के मुहावरे का ही रूपक था। उनके नेतृत्व में एनएसई, जो खुद एक नियामक संस्था है, अपने उपभोक्ताओं के साथ आपराधिक छल छद्म करता रहा और उस पर नजर रखने वाली सेबी भी अपनी नियामक भूमिका भूलकर आंखें मूदे रही।
लोकसेवकों के भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनी संस्थाओं के हाथ-पैर कैसे बांध दिए जाते हैं, इसके सबसे बड़े उदाहरण राज्यों के विजिलेंस संगठन हैं। कुछ राज्यों में एक निश्चित रैंक से ऊंचे अफसरों के खिलाफ कोई जांच बिना सरकार की इजाजत के नहीं हो सकती। यह इजाजत कितनी मुश्किल से मिलती है, इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि विभिन्न सरकारों के पास हजारों की संख्या में जांच के प्रस्ताव लंबित हैं। उत्तर प्रदेश विजिलेंस संगठन में काम करते समय मैंने पाया कि किसी लोकसेवक के खिलाफ जांच शुरू होने और अदालत में चार्जशीट दाखिल करने के क्रम में आधा दर्जन से अधिक चरणों की अनुमति के लिए सरकार के पास जाना पड़ता है और किसी भी स्वीकृति को हासिल करने में महीनों से लेकर सालों तक समय लग सकता है। यदि लोकसेवक पहुंच वाला हो, तो यह स्वीकृति कभी नहीं आती। नेकनीयत लोकसेवकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए रक्षा कवच भ्रष्ट अधिकारियों की हिफाजत के लिए काम आते हैं। दिलचस्प यह है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के तहत कार्रवाई करने वाली एजेंसियां एक ही मामले में अलग-अलग मापदंडों से कार्रवाई करती हैं। मसलन, एक सामान्य पुलिस थाने को, जिसके पास संसाधन व विशेषज्ञता कम है, अपने से ज्यादा बेहतर सुसज्जित विजिलेंस संगठनों के मुकाबले सरकार के पास इजाजत के लिए कम दौड़ना पड़ता है, क्योंकि उन्हें आईपीसी या सीआरपीसी से सीधे अधिकार मिले हुए हैं, जबकि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बने कानून और प्रक्रियाएं विजिलेंस से जुड़ी संस्थाओं के सामने कदम-कदम पर रुकावटें खड़ी करती हैं।
पिछले दिनों नोएडा में 32 मंजिला जुड़वां इमारतों को अदालती आदेश के चलते गिरा दिया गया। एक बार गिर जाने के बाद यह तो साबित हो ही गया कि इनका निर्माण भ्रष्टाचारी लोकसेवकों की मिलीभगत से ही संभव हुआ था, फिर भी वर्षों बाद भी उन्हें जेल नहीं भेजा जा सका और उबाऊ प्रक्रियाओं में जांच लंबित रही। राजधानी दिल्ली के ठीक बगल में घटित यह बड़ा मामला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन इमारतों के बगल से गुजरने वाली सड़क से रोज वे लोग गुजरते रहे, जिनकी जिम्मेदारी इनके निर्माण को रोकने की थी और वे अपनी आंखें मूंदे रहे। हमारे तंत्र में उत्तरदायित्व निर्धारित करने की स्वत:स्फूर्त प्रक्रिया का अभाव ही इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अडानी समूह की कंपनियों की गिरावट का वित्तीय संस्थाओं पर बुरा असर पड़ा, तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा देश के आम निवेशकों को भुगतना पड़ेगा। यह एक स्वाभाविक सवाल हो सकता है कि उनके तरक्की के ग्राफ को अस्वाभाविक रूप से ऊपर बढ़ते देखकर भी नियामक संस्थाएं क्यों नहीं चेतीं?
हाल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा सीट बेल्ट न बांधने के जुर्म में लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जुर्माना ठोक दिया था या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के घर की तलाशी लेकर एफबीआई ने कई ऐसे गोपनीय दस्तावेज बरामद कर लिए हैं, जिनको उनके घर में नहीं होना चाहिए था। यह सब शायद इसीलिए संभव हो सका कि इन मुल्कों में नियामक संस्थाएं स्वतंत्र हैं। हमें भी अपनी नियामक संस्थाओं को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त और उत्तरदायित्व के संस्थागत अंतर्निहित प्रावधानों वाला बनाने के बारे में सोचना होगा।
Date:07-02-23
भारतीयों की थाली में क्या फिर लौट आएंगे मोटे अनाज
मनु जोसफ, ( पत्रकार और उपन्यासकार )
भारत का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेहतरीन भोजन के रूप में मोटे अनाज की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुमोदन में मेज थपथपाई और शेष संसद हर्ष में शामिल हो गई, मानो वे सभी इन प्राचीन मोटे अनाजों के शौकीन हों।
वैसे, भारत इन दिनों कुछ दिलचस्प काम कर रहा है। भारतीयों व बाकी दुनिया को वह स्वास्थ्य सलाह की पेशकश कर रहा है। भारत लोगों से मोटे अनाज खाने को कह रहा है। वैसे इसकी मुख्य प्रेरणा तो इन अनाजों से अधिक धन कमाना प्रतीत होता है, क्योंकि भारत मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत सरकार भी इन अनाजों को सेहत के अनुकूल मानती है। भारतीय राष्ट्रवादी सोचते हैं कि जो कुछ भी प्राचीन है, वह हमारे लिए अच्छा है। ऐसे में, मोटे अनाज ‘महान’ घोषित होने की राह पर हैं। हालांकि, इस दलील में अतिशयोक्ति शामिल है। विचार करना चाहिए कि क्या मोटे अनाज को अपनाने में देर नहीं हो गई है? क्या ये अनाज अब मान्यता के लायक हैं? हां, ये चावल और गेहूं की तुलना में अधिक स्वास्थ्यकर हैं, इसलिए इनका ढिंढोरा पीटा जा रहा है।
वैज्ञानिक दृष्टि से मोटे अनाज एक प्रकार की घास के फल होते हैं; उन्हें घास के बीज या बीज वाले फल भी माना जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या खाते हैं, इसका अधिकांश हिस्सा हमारे पेट में ग्लूकोज बन जाता है और हमारे खून में मिल जाता है। ग्लूकोज शुगर या शर्करा का एक सरल रूप है। जितनी जल्दी कोई भोजन शुगर बनता है, उतना ही वह हमें आकर्षित करता है। किसी भी पौधा-आधारित भोजन की व्यावसायिक सफलता शर्करा वितरण पर निर्भर करती है, इसीलिए हमारे समय के सबसे सफल अनाज चावल और गेहूं हैं। अनाजों की दौड़ में चावल और गेहूं इसलिए विजयी हुए, क्योंकि उनकी आधुनिक किस्में स्वादिष्ट हैं; इसके अलावा ज्यादा चबाने-पकाने की असुविधा के बिना बहुत परिष्कृत रूपों में इनका सेवन किया जा सकता है।
आधुनिक दुनिया मीठे की गुलाम है। कोई भी धर्म या परंपरा या यहां तक कि मां का प्यार भी मिठास के बिना नहीं चल सकता। लोग अपनी लत के लिए शुगर लॉबी को दोष देते हैं, मानो ‘उबली गोभी लॉबी’ होती, तो सब उबली गोभी ही खा रहे होते? कुल मिलाकर, भारत में शुगर से बचाव आसान नहीं। आधुनिक चावल व गेहूं की सफलता का नतीजा है कि ये बहुत अच्छे शुगर-वितरण साधन हैं। इन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को अत्यधिक शर्करा से भर दिया है। चावल और गेहूं की तुलना में मोटे अनाज हमारे अंदर बहुत धीरे-धीरे ग्लूकोज में तब्दील होते हैं, इसलिए ये स्वास्थ्य के अनुकूल माने जाते हैं।
स्वस्थ भोजन क्या है? यह गंभीर विवाद का क्षेत्र है। फिलहाल, मेरा जोर इस बात पर है कि शरीर में शर्करा बनने की प्रक्रिया को धीमा कैसे किया जा सकता है? चावल व गेहूं में भी फाइबर होता है, पर मोटे अनाजों में ज्यादा होता है। फाइबर भोजन के ग्लूकोज में रूपांतरण को धीमा कर देता है। शरीर की इस व्यवस्था का सबसे अच्छा विवरण मुझे हरमन पोंटजर की किताब बर्न : द मिसअंडरस्टूड साइंस ऑफ मेटाबोलिज्म में मिला है, जिसके मुताबिक, फाइबर आंतों की दीवारों पर एक जाली जैसा फिल्टर बनाता है, जो शर्करा के अवशोषण को धीमा कर देता है व रक्त-प्रवाह में पोषक तत्वों के लिए ज्यादा जगह बनती है।
फाइबर लोगों को परिपूर्णता का एहसास कराता है, जिससे लोग कम खाते हैं। इसके अलावा, आम तौर पर लोग रेशेदार की तुलना में अन्य अनाज व सब्जियों का स्वाद ज्यादा पसंद करते हैं। इसी से मुझे लगता है, भारत में मोटे अनाज का प्रचार अधिक सफल नहीं होगा। दुनिया ने हमेशा दिखाया है कि लोग स्वास्थ्य के बारे में बात तो खूब करते हैं, लेकिन स्वादिष्ट भोजन को ही तरजीह देते हैं। गरीब जैसे ही कुछ पैसे वाले होते हैं, तो मोटे अनाज को छोड़ देते हैं। सदियों से यही होता आया है। बेशक, मोटे अनाज जीवित रहेंगे, पर उनका अलग आला बाजार होगा। मोटे अनाजों का ज्यादा प्रचार उनके उपयोग को विभिन्न प्रयोगों के जरिए खराब करेगा। ऐसा होने भी लगा है।
