
विविधता में एकता
Date:05-03-20 To Download Click Here.
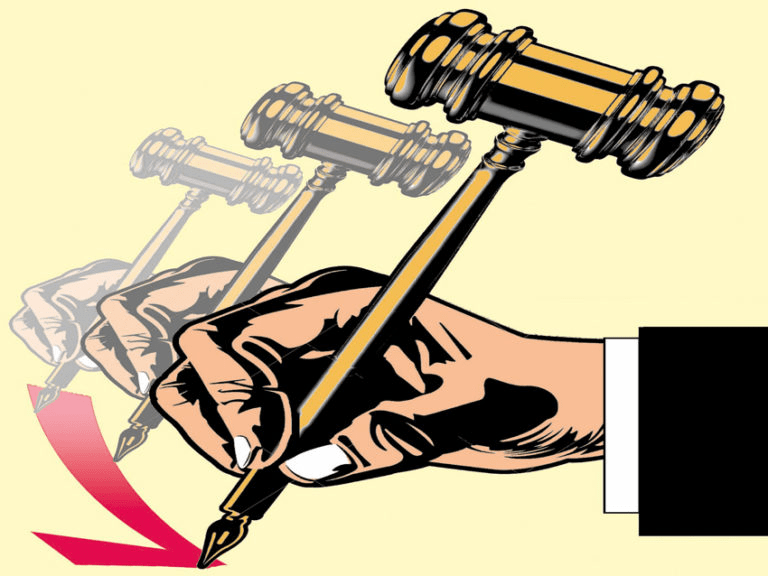
19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, राजा राम मोहन राय ने प्रेस पर पाबंदियों के खिलाफ विरोध किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि एक सरकार को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, और उन्हें वे साधन उपलब्ध कराने चाहिए, जिनके द्वारा वे अपने विचारों को सुगमता और सहजता से संप्रेषित कर सकें। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
नागरिक स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता सीधे वैसे ही प्रवाहित होती है, जैसा कि राज्य का असहमतियों के प्रति व्यवहार होता है। कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध सरकारी तंत्र, शांतिपूर्ण और वैध विरोध-प्रदर्शनों पर रोक लगाने को नियोजित नहीं है। उसका दायित्व है कि वह विचार-विमर्श के लिए स्थान दे। एक उदार लोकतांत्रित सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कानून के शासन के भीतर, वह अपने नागरिकों को हर कल्पनीय तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का आनंद लेने दे और प्रचलित कानूनों के खिलाफ विरोध और असंतोष व्यक्त करने का अधिकार दे।
शांतिपूर्ण विरोधों को ‘राष्ट्र‘-विरोधी’ या लोकतंत्र-विरोधी’ कहकर उनका दमन करना, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, और लोकतंत्र के संवर्धन के लिए हमारी प्रतिबद्धता के प्रतिकूल है। असंतोष या मतभेदों की रक्षा करना हमें यह याद दिलाता है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारें हमें विकास और सामाजिक समन्वय के लिए एक वैध उपकरण प्रदान करती हैं। वे हमारे बहुलवादी समाज को परिभाषित करने वाले मूल्यों और पहचान पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती हैं। विरोध-प्रदर्शनों को रोकने के लिए सरकारी तंत्र का प्रयोग करने से भय का वातावरण बनता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भयानक प्रभाव डालता है। यह कानून के शासन का उल्लंघन करता है, और बहुलवादी समाज के संवैधानिक दृष्टिकोण से हमें भटकाता है।
प्रश्नों और असंतोष के लिए स्थान को खत्म कर देने से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के आधार नष्ट हो जाते हैं। इस अर्थ में देखें तो असंतोष या मतभेद लोकतंत्र का सुरक्षा वॉल्व है। असंतोष और विरोधों को दबाना और भय का वातावरण उत्पन्न करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन और संवैधानिक मूल्यों का हनन करता है। यह उस संवाद-आधारित लोकतांत्रिक समाज के हृदय पर प्रहार करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान और विचार का प्रेरक है।
बहुलवाद की रक्षा के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जहाँ मतभेदों को शामिल किया जा सके, उनके साथ जिया जा सके और उसे सामाजिक व्यवस्था में स्थान दिया जा सके। अतः सरकारी तंत्र का यह दायित्व है कि वह अपनी मशीनरी का उपयोग कानून के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए करे, और किसी भी व्यक्ति द्वारा उस पर किए जाने वाले प्रहार को रोके। ऐसा करने का अर्थ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की न केवल रक्षा करना है, अपितु उसका स्वागत करना है, उसको बढ़ावा भी देना है। बहुलवाद को सबसे बड़ा खतरा मतभेदों और विरोधी दृष्टिकोणों के दमन से है। बौद्धिकता का दमन राष्ट्र की अंतरात्मा का दमन होता है।
देश की विविधता के संरक्षण के लिए बहुलवाद न केवल वचन देता है, बल्कि व्यक्तिगत और समान गरिमा प्रदान करने का आश्वासन भी देता है। इस अर्थ में बहुलवाद, संविधान के मूल सिद्धांतों का पोषण करता है, और राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य की सामग्री प्रदान करता है।
डॉ. अम्बेडकर ने इसके महत्व को जानते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि, ‘‘भाईचारे के बिना, स्वतंत्रता और समानता एक सामान्य भाव नहीं बन सकते। इसके अभाव में उन्हें लागू करने के लिए एक कांस्टेबल की आवश्यकता होगी।’’ बंधुत्व की अनुभूति तभी हो सकती है, जब एक ऐसा राष्ट्र हो, जहाँ विभिन्न समूह के लोग केवल सह-अस्त्वि ही नहीं; बल्कि सहिष्णुता, प्रेम, सम्मान और स्नेह का एक सामान्य सूत्र भी साझा करते हों। इसी के चलते टैगोर के राखी विरोध ने बंगाल का विभाजन होने से रोका था।
यह आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। विरासत में मिले समृद्ध बहुलतावादी इतिहास का संरक्षण करने की क्षमता हमारे पास है। समरूपता, भारतीयता की परिभाषा नहीं है। हमारे मतभेद हमारी कमजोरी नहीं हैं। मानवता को सर्वोपरि रखने की हमारी मान्यता में मतभेदों को पार करने की अपार शक्ति है। बहुलवाद का महत्व केवल इसलिए नहीं है, क्योंकि यह संविधान की दृष्टि से विरासत में मिला है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में इसके निहित मूल्य के कारण भी है।
भारत अपने आप में विविधता का एक उप-महाद्वीप है। यह सदियों से धर्म, भाषा और संस्कृति की जीवंत विविधता का देश रहा है। भारत के संदर्भ में बहुलवाद, औपनिवेशिक काल में ही अपनी जीत दर्ज कर चुका है। उस काल के अत्याचारों के सामने, संस्कृति के भिन्न खंडित हिस्सों से बाहर एक संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए मानवता का ऐसा वसीयतनामा हमें मिला, जिसे हर भारतीय दूसरे भारतीय में देखता है।
हमारे राष्ट्र का सतत् अस्तित्व, हमें बताता है कि हम एक दूसरे की त्वचा के रंग, भाषा और ईश्वर को दिए गए नाम से परे आनंद की साझा खोज करते रहते हैं। ये ही वे संकेत हैं, जो भारत को बनाते हैं। एक कदम पीछे लौटते हुए हम देखते हैं कि वे किस प्रकार मानवीय करूणा और प्रेम का सतरंगी रूप बनाते हैं। बहुलवाद, विविधता को बर्दाश्त करने का वाद नहीं है, बल्कि वह तो इसका उत्सव है।
‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित न्यायाधीश अनंजय वाई. चंद्रचूड़ के लेख पर आधारित। 21 फरवरी, 2020