
12-04-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:12-04-23
Date:12-04-23
Build The Answer
Ladakh or Arunachal, India’s counter to China’s border tactics must be via capability enhancement
TOI Editorials
India-China border tensions appear to be moving east as New Delhi and Beijing trade verbal salvos over Arunachal Pradesh. Amit Shah’s visit to the northeastern state not only saw him launch GoI’s Vibrant Villages Programme but also reiterate the point about defending every inch of Indian territory. Unsurprisingly, Beijing protested by asserting its so-called claims over ‘south Tibet’.
The larger geopolitical context is this: while Indian and Chinese troops continue to be engaged in their border standoff in eastern Ladakh, Beijing wants New Delhi to normalise relations and compartmentalise the border dispute. The truth is Beijing has no interest in resolving the border row since it enjoys considerable natural military advantages along the LAC. The latter have been further reinforced since the 2020 Galwan clashes through fresh construction of roads, bridges and helipads on the Chinese side. And as China prepares for an intensification of the strategic competition with the US and the Quad, it wants to hold the border dispute as leverage over India. Thus, India has no choice but to rapidly reduce the border infra gap to prevent further Chinese salami chopping. Beijing understands strength. It’s true that GoI has quickened the pace of infra development. But more needs to be done. The VVP scheme is a wellintentioned attempt at preventing out-migration from remote border villages to make them natural defences. But its success will depend on speed and quality of implementation.
Bear in mind that as the birthplace of the sixth Dalai Lama, Arunachal assumes salience for China’s Tibet question. India must start preparing for future tussles over the declaration of the next Dalai Lama. Countering China will require a multidimensional approach.
Building safeguards
Misuse of detention power renders need to stick to procedure paramount
Editorial
The Supreme Court’s observation that preventive detention laws are a colonial legacy and confer arbitrary powers on the state is one more iteration of the perennial threat to personal liberty that such laws pose. For several decades now, the apex court and High Courts have been denouncing the executive’s well-documented failure to adhere to procedural safeguards while dealing with the rights of detainees. While detention orders are routinely set aside on technical grounds, the real relief that detainees gain is quite insubstantial. Often, the quashing of detention orders comes several months after they are detained, and in some cases, including the latest one in which the Court has made its remarks, after the expiry of the full detention period. Yet, it is some consolation to note that the Court continues to be concerned over the misuse of preventive detention. In preventive detention cases, courts essentially examine whether procedural safeguards have been adhered to, and rarely scrutinise whether the person concerned needs to be detained to prevent prejudice to the maintenance of public order. Therefore, it is salutary that the Court has again highlighted that “every procedural rigidity, must be followed in entirety by the Government in cases of preventive detention, and every lapse in procedure must give rise to a benefit to the case of the detenu”.
Some facts concerning preventive detention are quite stark: most detentions are ultimately set aside, and the most common reason is that there is an unexplained delay in the disposal of representations that the detainees submit against their detention to the authorities. Failure to provide proper grounds for detention, or delay in furnishing them, and sometimes giving illegible copies of documents are other reasons. In rare instances, courts have been horrified by the invocation of prevention detention laws for trivial reasons — one of the strangest being a man who sold substandard chilli seeds being detained as a ‘goonda’. An unfortunate facet of this issue is that Tamil Nadu topped the country (2011-21) in preventive detentions. One reason is that its ‘Goondas Act’ covers offenders who range from bootleggers, slum grabbers, forest offenders to video pirates, sex offenders and cyber-criminals. The law’s ambit is rarely restricted to habitual offenders, as it ought to be, but extends to suspects in major cases. Across the country, the tendency to detain suspects for a year to prevent them from obtaining bail is a pervasive phenomenon, leading to widespread misuse. Preventive detention is allowed by the Constitution, but it does not relieve the government of the norm that curbing crime needs efficient policing and speedy trials, and not unfettered power and discretion.
इस फैसले से न्यायालयों का बोझ कुछ कम होगा
संपादकीय
विगत संविधान दिवस पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा था कि ओडिशा और झारखंड में अनेक गरीब विचाराधीन कैदी इसलिए वर्षों से जेल में है क्योंकि वे जमानत राशि जमा नहीं कर सकते। उन्होंने पूछा कि ऐसे में ज्यादा जेल बनाने की जगह क्या उन्हें छोड़ा जाना उचित नहीं होगा? इसके बाद वित्तमंत्री ने बजट भाषण में बताया कि सरकार ऐसे लोगों की जमानत राशि देने की स्कीम लाएगी। अब गृहमंत्रालय ने नई स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य सरकारों को यह राशि इस आशय के साथ दी जाएगी कि वे गरीब विचाराधीन कैदियों की पहचान कर उन्हें रिहा करने का प्रबंध करें। एनसीआरबी के अनुसार देश की जेलों में तीन लाख 71 हजार से ज्यादा विचाराधीन कैदी बंद हैं। इनमें से अधिकांश वर्षों से जमानत न देने के कारण दिला नहीं हो पा रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा था कि केवल इस वर्ग के कैदियों के मामले निपटाने में देश की कोट्र्स को 700 वर्ष लगेगे। आज भारत में चार में से हर तीन कैदी इस वर्ग के हैं जबकि वैश्विक औसत तीन में एक का है। इसमें हर माह 5 हजार व कैदी और जुड़ जाते हैं। 54 कामनवेल्थ देशों (जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं) में जों की दी हुई समान अपराध न्याय प्रणाली है। इनमें से बांग्लादेश में इस वर्ग के कैदी 80% हैं। इसके बाद भारत का स्थान है। एक लोकतांत्रिक देश के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है कि जेलों में 76% ऐसे लोग बंद है, जिन पर अभी कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि इनमें से अधिकांश गरीबी के कारण जमानत मिलने के बावजूद बांड न भर पाने के कारण बंद हैं। नई योजना सराहनीय कदम है।
Date:12-04-23
बदलते मौसम के असर से खेती पर संकट
अंशुमान तिवारी, ( मनी-9 के एडिटर )
इतिहास हमारे लिए ज्यादा मूल्यवान है? हजार दो हजार साल पुराना वाला या कि जो हमारे सबसे करीब का है? किसी समाज के लिए वह इतिहास शायद ज्यादा प्रासंगिक है, जिससे उसका भविष्य प्रभावित होता है। आइए मिलिए अपने करीब इतिहास से जिसे हम गढ़ रहे हैं। यह इतिहास हमारे वर्तमान में पैर में कील की तरह धंस गया है। भारत की अर्थव्यवस्था के पैरों में कील का असर कुछ ज्यादा ही गहरा है। बीते साल जल्दी आई गर्मी गेहूं (रबी) की फसल चाट गई थी। फिर मानसून के दौरान शुरुआती सूखे और बाद की बाढ़ ने खेती को तितर-बितर कर दिया। अब गर्मी का तूफान यानी एल निनो आ रहा है। मानसून संकट में होगा। सूखे की मुनादी बजने लगी है। 2008 और 2014 की डरावनी यादें लौट रही हैं। यही तो है हमारा सबसे करीब इतिहास मौसम के असर से खेती एक बड़े संकट से मुकाबिल है!
साझा ताजा इतिहास
अमेरिकी ओश्नोग्राफिक एजेंसी और ग्लोबल कार्बन एटलस ने बताया कि 2010 से 2019 का दशक 140 साल के दर्ज – इतिहास में सबसे गर्म था। इसमें भी 2019 में मानव इतिहास में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज हुआ और समुद्री तापमान में भी रिकार्ड बढ़ोतरी हुई। बीते 30 साल में समुद्रीय जलस्तर दोगुना हो गया है। पर्यावरण पर अंतरसरकारी पैनल ने 2022 तक तापमान बढ़त को 1.09 डिग्री पर रोकने का लक्ष्य रखा था। यह संकल्प कब का टूट चुका है।
आपदाओं का अर्थशास्त्र
भयावह आंकड़े उगल रहा है। 2022 में दुनिया को पर्यावरणीय आपदाओं से 360 अरब डॉलर का नुकसान हुआ । विश्व के प्रमुख रिइंश्योरेंस ब्रोकर गैलगर ने बताया कि इसमें केवल 140 अरब डॉलर के नुकसानों का बीमा था। इसके बाद जो डूबा सो गया। अमेरिका के नेशनल एनवायरमेंट सेंटर का आकलन है कि अकेले अमेरिका में ही वर्ष 2022 में करीब 18 आपदाओं में प्रति संकट एक अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। अमेरिका से बाहर बीते साल की सबसे बड़ी आपदा पाकिस्तान की बाढ़ थी, जिससे 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। की कोई सुरक्षा नहीं थी। भारत में तो फसल बीमा ही अभी कायदे से उगा नहीं। जोशीमठ के पहाड़ों से लेकर मैदानी खेतों तक गुस्साई हुई प्रकृति जीविका को निगल रही है।
काहे का सामान्य मानसून
खेती जीडीपी में 15 फीसदी का हिस्सा रखती है मगर 45 फीसदी आबादी को रोजगार देती है। मौसम के असर से भारत की खाद्य सुरक्षा की बुनियाद में तीन बड़ी दरारें पड़ गई हैं। एक बार बार बढ़ने वाली गर्मी और पानी की कमी, दूसरी अचानक होने वाली भारी बारिश और तीन- उपजाऊ मिट्टी का क्षरण । सामान्य मानसून अब कहीं से भी सामान्य नहीं है। जैसे 2022 में शुरुआत के वक्त मानसून सामान्य था, लेकिन खरीफ की बुवाई के मौसम में पूरी कृषि-पट्टी आंशिक सूखे से जूझती रही। बुवाई में देरी हुई। मानसून की देर वापसी दोहरी मुसीबत है। बीते साल उत्तर की अनाज पट्टी के कई इलाकों में मानसून देर से आया और जाते-जाते भारी बाढ़ छोड़ गया। मानसून की यह तुनकमिजाजी फसलों की बुवाई और कटाई (हार्वेस्ट) दोनों को उलट-पुलट कर देती है। इससे पूरा चक्र बिगड़ गया। क्रिसिल के एक अध्ययन में यह भी पता चला कि सामान्य बारिश वाले इलाकों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। जरूरत से कम और ज्यादा बारिश स्थाई हो चली है। बीते कुछ वर्षों में सितम्बर- अक्टूबर की बाढ़ एक तरह से नियम बन गई है। मानसून के समाप्त पर होने वाली वर्षा मौसम के औसत से 47 फीसदी ज्यादा है।
आ गया सूखा गले तक
वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 बताती है कि उत्तर प्रदेश के गेहूं से लेकर दार्जीलिंग में चाय की खेती तक मौसम ही बड़ी मुसीबत है। पर्यावरण पर अंतरराष्ट्रीय अंतरसरकारी समिति का आकलन है कि 21वीं सदी में तापमान में एक से चार डिग्री की बढ़त से भारत में धान के उत्पादन में 10 से 30 फीसदी और मक्का की पैदावार में 25 से 70 फीसदी की कमी आएगी। 2018 में सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में बताया था कि पर्यावरण में बदलाव से अगले 25 से 30 सालों में भारत की कृषि आय में 18 फीसदी तक की कमी हो सकती है। गैर-सिंचाई वाले इलाकों में कमाई 25 फीसदी घट जाएगी। बीते बरस फसल तो बच गई, लेकिन भोजन की महंगाई ने नहीं छोड़ा।
कहां है सुरक्षा कवच
सरकारों को तत्काल अनाज भंडारण में बड़ा निवेश करना होगा, क्योंकि अब मौसम का कोई भरोसा नहीं रह गया है। प्रसंस्करण की मदद से मौसमी खाद्य महंगाई को सम्भाला जा सकता है मगर टैक्स तो कम हों। कृषि शोध में तत्काल बदलाव करने की जरूरत है। ऊंचे तापमान पर जल्दी तैयार होने वाले अनाज दलहन और सब्जियों की नई पीढ़ी चाहिए। भारत ने पिछले साल पांच तूफानों का सामना किया, जिनमें तीन बड़े व्यापक असर वाले थे। जर्मनवॉच ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स और काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट बताती हैं कि 1970 से 2019 के बीच भारत में पर्यावरण की आक्रामकता में अभूतपूर्व बढ़त हुई है। भारत उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है, जहां पर्यावरण सबसे मारक हो चला है। अप्रत्याशित घटनाओं के खतरे के सूचकांक में भारत अब शीर्ष 20 देशों में शामिल है। अर्थव्यवस्था के विकास के सभी ख्वाबों पर मौसम भारी पड़ने वाला है। इस आह को असर होने के लिए एक उम्र नहीं चाहिए। भोजन का खर्च या ग्रॉसरी का बिल देखिए, असर शुरू हो चुका है!
बेटियों की सेहत
संपादकीय
देश में हाशिये के तबकों के परिवारों की बच्चियों के स्कूलों तक पहुंच सकने के कितने स्तर रहे हैं, उनकी राहों में क्या बाधाएं रही हैं, यह जगजाहिर है। आजादी के बाद से समय-समय पर सरकारों ने लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई को लेकर कई तरह की योजनाएं लागू कीं, नीतिगत फैसले किए। लेकिन आज भी कई ऐसे पहलू छूटे हुए हैं, जिनकी वजहों पर गौर करना बहुत जरूरी नहीं समझा गया और जिनके चलते बड़ी तादाद में स्कूली छात्राएं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। ये वजहें स्कूली पढ़ाई-लिखाई में गुणवत्ता के सवालों से इतर कुछ ऐसी स्थितियों से जुड़ी हो सकती हैं, जिन्हें निजी समस्याओं के तौर पर देखा जाता है, मगर वे स्कूली लड़कियों के जीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। मसलन, स्कूलों में लड़कियों के लिए साफ-सुथरे शौचालय से लेकर माहवारी जैसे कुछ बिंदु उनके लिए विशेष इंतजाम की जरूरत को रेखांकित करते हैं। इस लिहाज से देखें तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह नोटिस जारी करना बेहद अहम है, जिसके तहत माहवारी स्वच्छता को लेकर एक स्पष्ट नीति बनाने का निर्देश दिया गया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि स्कूलों में छठी से बारहवीं की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड दिया जाए और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की जाए। अनेक अध्ययनों में यह रेखांकित किया गया है कि स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच की कमी और माहवारी से जुड़े सामाजिक व्यवहार के कारण बहुत सारी लड़कियां स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। शिक्षा की सूरत बदलने को लेकर सरकारें समय-समय पर अनेक नीतिगत फैसले लेती रही हैं और नए कार्यक्रमों की घोषणा करती रही हैं। लेकिन गुणवत्ता आधारित शिक्षा के सवाल के अलावा एक अहम पहलू यह है कि अगर इसमें लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई निर्बाध जारी रहने के लिए जरूरी कारकों पर गौर करने के साथ इसमें मौजूदा कमियों को दूर नहीं किया जाता है तो कोई बेहद अहम पहलकदमी भी आधे-अधूरे नतीजे देगी। यह सभी जानते हैं कि किशोरावस्था में लड़कियों को सेहत से जुड़ी किन जटिलताओं का सामना करना पड़ता है और उसके क्या कारण रहे हैं।
सच यह है कि आबादी के एक बड़े तबके के बीच सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से पार निकल कर किसी तरह स्कूल पहुंची लड़कियां माहवारी से उपजी दिक्कत, पीने के साफ पानी और शौचालय जैसी बुनियादी जरूरतों के अभाव से दो-चार होती हैं। माहवारी में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी प्रशिक्षण और संसाधनों के अभाव के चलते वे अपेक्षित सावधानी नहीं बरत पातीं। इसी तरह, स्कूलों में अलग शौचालय का अभाव उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है। इसलिए स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था करने के साथ-साथ कम कीमत वाले सैनिटरी पैड मुहैया कराने पर एक समान नीति वक्त का तकाजा है। इसके समांतर, सरकार को इस सामाजिक जड़ता को दूर करने के लिए भी नीतिगत पहल करने की जरूरत है, जिसके तहत कई समुदायों में आज भी माहवारी को लेकर नकारात्मक धारणाएं हैं। इसका खमियाजा आखिर लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है। दरअसल, कई बार दिखने में पारंपरिक चलन या सामान्य मानी जानी जाने वाली बातें समाज के एक बड़े हिस्से के लिए वंचना का काम करती हैं और यहां तक कि इनकी वजह से उनके अधिकारों का भी हनन होता है। इसलिए ऐसे मामूली दिखने वाले बिंदुओं पर भी गौर करके उसकी जटिलता को दूर करना एक लोक कल्याण का दावा करने वाली सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
Date:12-04-23
आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद छोटे उद्यम
सत्येंद्र किशोर मिश्र
आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी, बेरोजगारी, प्रतिव्यक्ति निम्न आय, निरक्षरता और औद्योगिक पिछड़ेपन की जकड़ में थी। यह स्वीकृत तथ्य है कि औद्योगीकरण के जरिए आर्थिक विकास की मजबूत बुनियाद पर बेहतर सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। दो हजार वर्षों से अधिक का भारतवर्ष का गौरवशाली आर्थिक संपन्नता का इतिहास दरअसल, लघु उद्योगों के रूप में उद्यमिता, हस्तशिल्प और कौशल की परंपरा ही थी। भारत में नियोजन के शुरुआती दौर में लघु उद्योगों को नजरंदाज कर, बड़े उद्योगों के जरिए औद्योगिक विकास की कोशिशें तो उसके अच्छे नतीजे भी दिखे। बाद में उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के कारण बाजारवाद, निजीकरण और प्रतिस्पर्धी माहौल भी सामने आया। बड़े और भारी उद्यागों की सीमाएं भी दिखीं। गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मामलों में विफल साबित हुए। अनुकूल पूंजी-उत्पाद अनुपात तथा रोजगार की ऊंची संभावनाएं लघु उद्योगों की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। शायद बहुत देर से औद्योगिक विकास में लघु उद्योगों की भूमिका को पहचानते हुए, इसके विकास की कोशिशें हुर्इं। समझना होगा कि ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की संकल्पना में इसे रफ्तार देने की जरूरत है।लघु उद्योग, आर्थिक विकेंद्रीकरण कर आय तथा संपत्ति की असमानताओं के साथ-साथ भौगोलिक असंतुलन को कम करते हैं। उपभोक्ताओं को विविधता और विकल्प उपलब्ध कराते हैं। स्थानीय ज्ञान और कौशल, कलात्मकता का कम पूंजी के साथ उपयोग करते हैं, साथ ही बड़े उद्योगों के सहायक उद्यम का भी कार्य करते हैं। भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई को ‘विकास का इंजन’ और ‘अर्थव्यवस्था का पावरहाउस’ जैसे विशेषणों से नवाजा जाता है। समावेशी विकास में शायद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका एमएसएमई क्षेत्र की हो सकती है। आज भारत में सवा छह करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाइयों में ग्यारह करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त है। एमएसएमई की जीडीपी में तीस फीसद तथा निर्यात में अड़तालीस फीसद से अधिक योगदान के साथ आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। एमएसएमई कुल औद्योगिक इकाइयों में पंचानबे फीसद से अधिक हिस्से के साथ भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति की बुनियाद है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की लगभग 6.34 करोड़ इकाइयों में से विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों का जीडीपी में 6.11 फीसद, सेवा क्षेत्र की इकाइयों का जीडीपी में 24.63 फीसद तथा सकल विनिर्माण उत्पादन में 33.4 फीसद योगदान है। एमएसएमई क्षेत्र ग्यारह करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ भारत के कुल निर्यात में लगभग अड़तालीस फीसद योगदान करता है। लगभग इक्यावन फीसद एमएसएमई इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यबल को संयोजित होने का अवसर उपलब्ध होता है। कुल एमएमएमई उद्यमों में निन्यानबे फीसद से अधिक सूक्ष्म उद्यम हैं। समावेशी विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में इनकी विशेष भूमिका है। भारत में विशाल असंगठित कार्यबल को देखते हुए रोजगार की दृष्टि से एमएमएमई क्षेत्र की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
मगर पिछले कुछ वर्षों से एमएसएमई क्षेत्र लगातार अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं झेल रहा है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान इस क्षेत्र में रोजगार तथा विक्रय राजस्व में काफी गिरावट आई। कच्चे माल की लागतों में तीस से पचास फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि यह क्षेत्र महामारी से पूर्व के स्तर तक पहुंचने को अब भी प्रयासरत है। अधिकांश एमएसएमई के पास लागतों में बढ़ोतरी की भरपाई करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। बावजूद इसके, एमएसएमई क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए औद्योगीकरण की ओर बढ़ रहा है। एमएसएमई क्षेत्र वैश्विक बाजार, डिजिटल कौशल विकास तथा किफायती उद्यम प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धी बाजार में खुद को स्थापित करने को तत्पर है।
एमएसएमई क्षेत्र का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरत है, जो इसे वैश्विक आर्थिक संकटों तथा प्रतिकूलताओं को झेलने में ताकत तथा जुझारूपन प्रदान करता है। देश भर में इक्यावन फीसद एमएसएमई इकाईयां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और बाकी उनचास फीसद नगरीय क्षेत्रों में स्थित हैं। यानी, लगभग सवा तीन करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शेष 3.09 करोड़ इकाइयां नगरीय क्षेत्र में स्थापित हैं। सर्वाधिक 2.3 करोड़ एमएसएमई इकाइयां व्यापार में लगी हुई हैं। विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 1.97 करोड़ एमएसएमई इकाइयां उत्पादक कार्यों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास में योगदान कर रही हैं। इस क्षेत्र की अस्सी फीसद इकाइयां पुरुषों के स्वामित्व में हैं और इसके मात्र पांचवें हिस्से का स्वामित्व महिलाओं के पास है।
एमएसएमई इकाइयों में से लगभग आधे पर स्वामित्व ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्ग का है, जबकि अन्य के स्वामित्व में लगभग एक तिहाई है। अनुसूचित जाति के स्वामित्व में 12.45 फीसद तथा अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व में मात्र 4.10 फीसद एमएसएमई इकाइयां हैं। सबसे खराब स्थिति अनुसूचित जनजाति की है, विशेषकर नगरीय क्षेत्र में मात्र 1.43 फीसद एमएसएमई इकाइयों का मालिकाना हक यानी उनका संचालन अनुसूचित जनजाति के हाथों में हैं।एमएसएमई इकाइयों के बढ़ते आकार के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी का हिस्सा घटता हुआ है। मध्यम आकार की एमएसएमई इकाइयों में ओबीसी का स्वामित्व 23.85 फीसद, अनुसूचित जनजाति का 1.09 फीसद तथा अनुसूचित जनजाति का अमूमन शून्य है। सूक्ष्म तथा लघु एमएसएमई के जरिए औद्योगीकरण को बढ़ावा देकर न केवल असंगठित क्षेत्र में रोजगार की दशा और दिशा सुधारी जा सकती है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक असमानता को भी कम किया जा सकता है।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण तथा एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र में कुल 11.10 करोड़ रोजगार में से विनिर्माण में 3.6 करोड़, व्यापार में 3.88 करोड़ तथा अन्य क्षेत्रों में 3.62 करोड़ लोग रोजगार में लगे हैं। अनुमानत: 6.31 करोड़ सूक्ष्म उद्यमों में 10.8 करोड़ व्यक्ति कार्यरत हैं, जो उद्योग में कुल रोजगार का लगभग सत्तानबे फीसद है। एमएसएमई क्षेत्र की 3.31 लाख लघु तथा 0.05 लाख मध्यम आकार की इकाइयों में क्रमश: 32 लाख (2.88 फीसद) तथा 1.8 लाख (0.16 फीसद) लोगों को रोजगार प्राप्त है।एमएसएमई क्षेत्र में नगरों में प्राप्त रोजगार की कुल संख्या 6.12 करोड़ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की संख्या 4.98 करोड़ से अधिक है। एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार का वितरण लिंगानुसार देखने पर पता चलता है कि तीन चौथाई से अधिक, 8.5 करोड़ पुरुषों को एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है, जबकि 2.7 करोड़ महिलाओं को, जो कि इस क्षेत्र में कुल श्रमबल के एक चौथाई से कम हैं। रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की सख्त जरूरत है।
स्वतंत्रता के बाद से लघु, सूक्ष्म और मझोले उद्योग एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, पर भारत के औद्योगीकरण में एमएसएमई का योगदान कभी एक-सा नहीं रहा है। शुरुआती दशकों में एमएसएमई क्षेत्र की उच्च रोजगार क्षमता को देखते-समझते हुए भी, उनकी भूमिका को सही ढंग से पहचाना नहीं जा सका। शायद भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके महत्त्व को समझा ही नहीं जा सका। जबकि एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए तेज और विशेष प्रयास की जरूरत थी। नए भारत में आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद एमएसएमई क्षेत्र ही बन सकता है। भारत के असंगठित क्षेत्र को सामाजिक-आर्थिक विकास का हिस्सा बनाने के लिए भी एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका को आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है।
चीन को तल्ख जवाब
संपादकीय

Date:12-04-23
जेल में भी जिंदगी से जद्दोजहद
सुशील देव
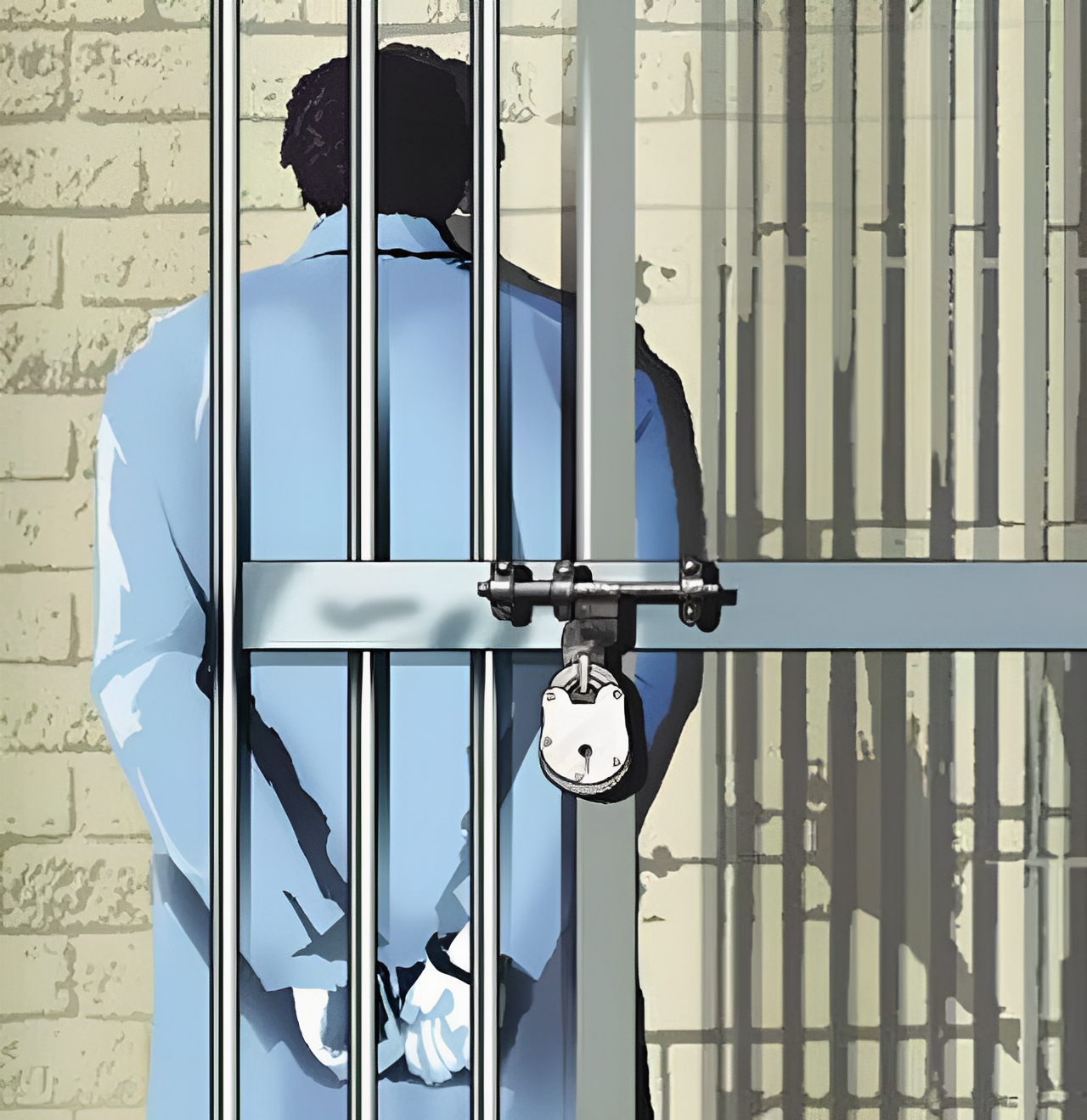
विशेषज्ञों के मुताबिक खास तौर पर विचाराधीन कैदियों का लंबे समय तक जेलों में बने रहना चिंता का विषय है। 1970 में राष्ट्रीय जेल जनगणना से पता चला था कि जेल के 52 फीसद कैदी मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब से धीरे-धीरे यह सिलसिला आगे ही बढ़ रहा है। यानी जेल में भीड़-भाड़ को कम करना है तो विचाराधीन कैदियों की संख्या को काफी कम करना होगा। भले ही यह अदालतों के बिना संभव नहीं, परंतु इस दिशा में न्याय प्रणाली के तीनों अंगों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोक सभा में जानकारी दी है कि देश भर की जेलों में बंद 1400 से अधिक कैदी अपनी सजा काटने के बाद जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं कर पाने की वजह से अभी भी जेलों में बंद हैं। इनकी रिहाई समय से हो जाती तो शायद जेलों का भार कम होता। गौरतलब है कि जेलों में कैदियों को क्षमता से ज्यादा रखने के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। यहां कैदियों की संख्या लगभग दोगुना है। दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की जेलें हैं। इन जेलों में कैदियों का बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा क्षमता से अधिक कैदी रखने वाले राज्यों में असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। मतलब साफ है कि कैदियों को जेलों में रखने में असंतुलन बड़े राज्यों में ज्यादा है। अगर हम दिल्ली के तिहाड़ की एक जेल, नंबर-4 की बात करें तो वहां 740 की जगह 3700 से अधिक कैदी बंद हैं। यहां नहाने-धोने या टॉयलेट जाने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। कई बार आपसी लड़ाई-झगड़े के कारण जेल प्रशासन को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। उन पर नजर रखने में संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी ओर कोरोना जैसी महामारी भी कई जेलों के लिए चिंता का सबब बन गई थी। एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में 80 प्रतिशत ऐसे कैदी हैं, जिन्हें अदालत से जमानत मिलने के बाद भी सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है। उनके पास जुर्माना के राशि चुकाने तक के पैसे नहीं। इस प्रकार दिल्ली में कुल 16 जेल हैं, जो करीब-करीब क्षमता से अधिक कैदियों से भरे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्डस ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक देश में कुल 1412 जेलों में अपने निर्धारित क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं। इसमें साल-दर-साल बढ़ोतरी ही होती जा रही है, जबकि जेलों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। सर्वोच्च अदालत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रामना के मुताबिक आज आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रिया ही सजा बन गई है। इस वजह से भी जेलों में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए अंधाधुंध गिरफ्तारी से लेकर जमानत हासिल करने में आ रही मुश्किलों के कारण विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक कैद में रखने की प्रक्रिया पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। अंडर ट्रायल के तौर पर कैदियों का सालों से बंद रहना उचित नहीं है। फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना व खुली जेल बनाना इसके उपाय हो सकते हैं। इसके अलावा कई न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की जरूरत है। दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में भारतीय जेलों में कैदियों की अपेक्षाकृत कम संख्या होने के बावजूद कई समस्याएं हैं। भीड़-भाड़, अंडर-ट्रायल, कैदियों की लंबे समय तक हिरासत, असंतोषजनक रहने की स्थिति, उपचार कार्यक्रमों की कमी और जेल कर्मचारियों के उदासीनता के कारण असंतुलन की स्थिति है। यहां तक कि अमानवीय नजरिए ने आलोचकों का ध्यान खींचा है। भारत में जेलों की स्थिति के बारे में देश के बाहर भी अच्छी छवि नहीं है।
कुल मिलाकर देश के जेलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ऐसे में सरकार को जेलों के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपराधी के रूप में कैद हैं, वह एक जीवित इंसान भी हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से और सम्मान से जीने का अधिकार है। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू इस मुद्दे पर अपना मत जता चुकी हैं कि जेलों में बहुत से लोगों को ना तो अपने मौलिक अधिकारों या कर्तव्यों के बारे में पता है, और ना ही संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानकारी। बाहर आने पर समाज द्वारा बुरे बर्ताव की चिंता उन्हें अलग सताती है। इसलिए जेलों की बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ पुनर्वास संबंधी उपयोगी कदम उठाना श्रेयस्कर होगा।
अपराध मुक्त राजनीति
संपादकीय
देश की विधायी संस्थाओं से आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को दूर करने की मंशा से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के संदर्भ में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो शपथ-पत्र दायर किया है, उसके गहरे निहितार्थ हैं। आयोग ने अपने हलफनामे में स्पष्ट कहा है कि वह राजनीति को पूरी तरह अपराध-मुक्त करने को प्रतिबद्ध है, पर वह प्रदत्त शक्तियों के दायरे में ही इससे संबंधित कदम उठा सकता है। प्रकारांतर से आयोग का यही कहना है कि उसके पास इतने कानूनी अख्तियार ही नहीं कि वह निर्णायक फैसले ले सके। जाहिर है, आला अदालत ने चार हफ्तों में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि जिन नेताओं के खिलाफ आरोप-पत्र दायर हो चुके हैं, या आरोप तय हो चुका है, उनके चुनाव लड़ने पर क्यों न रोक लगा दी जाए? आयोग ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई इस मांग के प्रति अपनी पूर्ण सहमति जताई है।
राजनीति के अपराधीकरण का मसला नया नहीं है। पिछले कई दशकों से इस संदर्भ में संसद से सड़क तक विमर्श होता रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं आया, बल्कि विधायी संस्थाओं में दागियों की आमद बढ़ती गई और तमाम पार्टियां नैतिकता को ताक पर रखकर जीतने की क्षमता के आधार पर ऐसे लोगों को टिकट बांटती रहीं। आलम यह है कि आज लोकसभा में बैठने वाले 43 फीसदी माननीयों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, तो वहीं उच्च सदन में बैठने वाले 39 प्रतिशत सदस्यों के विरुद्ध विभिन्न प्रकरणों में मामले लंबित हैं। देश की दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के 145 लोकसभा सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे सुनवाई के विभिन्न स्तरों पर हैं। निस्संदेह, देश की राजनीति को दागियों से निजात दिलाने के लिए तो संसद को ही कानून बनाना होगा, पर क्या ये पार्टियां ऐसा करेंगी? ऐसे में, सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। मगर यह भी देखना होगा कि राजनीतिक विद्वेष के तहत कई मुकदमे दायर किए जाते हैं। ऐसे में, त्वरित सुनवाई और गलत मुकदमे करने वालों को हतोत्साहित करने की जरूरत है।
बहरहाल, चुनाव आयोग की यह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि उसके पास सीमित कानूनी अधिकार हैं, मगर क्या यह सच नहीं है कि अपने सीमित अधिकारों के अधिकतम सदुपयोग से टीएन शेषन ने इस संस्था के लिए अभूतपूर्व प्रतिष्ठा अर्जित की? नजीर के तौर पर, आचार संहिता की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए थे, उससे उम्मीदवारों व राजनीतिक पार्टियों में भय पैदा हुआ था, दुर्योग से वह इन दिनों तिरोहित हो चला है! एक लोकतंत्र की कामयाबी का यह बुनियादी उसूल है कि उसमें सभी पक्षों को समान अवसर मिले, पर अब यह आम बात है कि कई चरणों में चुनाव के दौरान मतदान वाले इलाकों में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कुछ दल अपना प्रचार करते रहते हैं और आयोग के पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने और वोट मांगने के कारण चुनाव आयोग ने देश के एक दिग्गज नेता से छह वर्षों तक मताधिकार का अधिकार छीन लिया था। क्या आयोग को यह याद दिलाने की जरूरत है कि उसके पास आज भी कितने अहम अधिकार हैं? लोकतंत्र की सफलता लिखित कानूनों से अधिक सांविधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से तय होती है। चुनाव आयोग को यह भी याद रखना चाहिए।