
17-10-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
New dawn
Peace in West Asia hinges on resolution of Palestine issue
Editorial
While addressing the Knesset, the Israeli Parliament, U.S. President Donald Trump declared that the ceasefire agreement between Hamas and Israel, which he had helped broker, marked “the historical dawn of the new Middle East”. In Sharm el-Sheikh, Egypt, Arab and Muslim leaders joined him in praising his 20-point peace plan. While all sides hailed Mr. Trump’s role as a peacemaker, the declaration of a new era of peace in West Asia, claiming to end a “3,000-year-old” conflict, glosses over deep and enduring complexities. The Gaza ceasefire, which appears to be holding with Hamas and Israel releasing hostages and prisoners, is undoubtedly a relief for Palestinians and hostage families. But the greater challenge lies in implementing the next phase, let alone building “a new Middle East”. A notable outcome of the Sharm el-Sheikh summit was the joint declaration by Egypt, Qatar, Türkiye and the U.S., also calling for the safeguarding of the fundamental rights of Palestinians and Israelis. It recognised the region’s historical and spiritual significance to multiple faiths, and committed signatories to dismantling extremism and radicalisation. But the declaration was silent on more contentious issues — Hamas’s disarmament, one of the central objectives of the Trump plan, or of Israel’s continuing military presence in Gaza.
Mr. Trump later claimed that Hamas had promised to disarm, warning that “If they don’t disarm, we will disarm them…, perhaps violently”. But Israel, despite its two years in Gaza, has still failed to disarm Hamas. How then does Mr. Trump plan to disarm them? He also claimed that the Iran threat had been neutralised, and urged more Arab countries to join the Abraham Accords. While Iran’s regional influence has been dented, it remains an influential regional player. Hezbollah, despite military setbacks, continues to be a powerful socio-political actor within Lebanon, and U.S.-led attempts to disarm the Shia group have gone nowhere. In Yemen, despite relentless Saudi, American, British and Israeli bombing campaigns, the Houthis, another Iranian ally, still control key population centres, including Sana’a. Moreover, Arab countries now have growing security concerns about Israel, particularly after its bombing of Qatar in September. Against this background, Mr. Trump’s sweeping claims of regional peace ring hollow. What he should prioritise instead is ensuring that the Gaza ceasefire holds. The next step should be forcing Hamas to give up power in the enclave while pressing Israel to withdraw. Once peace is consolidated and reconstruction begins, the U.S., with its Arab and European allies, should work towards a practical road map for the establishment of a Palestinian state. Unless the Palestine question is resolved and the Israeli occupation ends, grand declarations about remaking the region will remain little more than empty rhetoric.
मैन्युफैक्चरिंग और प्रति- व्यक्ति आय पर फोकस हो
संपादकीय

सरकार को चुनिंदा आंकड़े देकर खुशफहमी पालने से बचना चाहिए। भारत को दुनिया में सबसे तेज विकास दर वाला देश बताने के पहले यह भी बताना होगा प्रति व्यक्ति आय या मानव विकास सूचकांक में हम दुनिया में पिछले अनेक दशकों से वहीं के वहीं हैं। जहां मंत्रालय का मानना है कि आने वाले एक-डेढ़ दशक तक अगर भारत 8% की विकास दर हासिल कर सके तो 2047 तक विकसित देशों में आ जाएगा, वहीं मॉर्गन स्टेनली की ताजा रिपोर्ट बताती है कि इस विकास दर से कुछ हासिल नहीं होगा। अगले दस वर्षों में 8.5 करोड़ नए युवा जॉब मार्केट में खड़े होंगे और अगर भारत को बेरोजगारी खत्म करनी है तो कम से कम 12.2% की दर से लगातार एक दशक विकास करना होगा। संकेत स्पष्ट हैं। मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में शेयर पिछले दस वर्षों में बढ़ने की जगह 16.7% से घटकर 15.9% रह गया है। तेज और संतुलित अर्थव्यवस्था तब कही जाती है, जब कृषि क्षेत्र से युवाओं का मैन्युफैक्चरिंग में स्थानापन्न हो सके। लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है और युवाओं का मजबूरन कृषि क्षेत्र में लौटना मैन्युफैक्चरिंग की लगातार गिरती स्थिति का परिचायक है। न भूलें कि टैरिफ की मार से भारत के 50 अरब डॉलर के अमेरिकी निर्यात पर भी असर पड़ने जा रहा है। देश में 17.7% युवाओं का बेरोजगार हो एक चिंतनीय आर्थिक परिदृश्य दिखाता है।
Date: 17-10-25
देशों में आपसी सहयोग के बिना दुनिया चल नहीं सकेगी
कौशिक बसु, ( विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट )
ये कठिन समय है। एक तरफ असमानता बढ़ रही है, वहीं कई देशों के राजनेता गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों और सेवाओं में कटौती कर रहे हैं। साथ ही वे प्रवासियों और शरणार्थियों के खिलाफ भय और क्रोध को भी भड़का रहे हैं।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, समृद्धि को बढ़ाना और नागरिकों की सुरक्षा के उनके कथित नेक इरादे खुद को और अपने धनी साथियों को समृद्ध बनाने के एजेंडे के लिए एक छद्म आवरण मात्र होते हैं। राजनीति के व्यवहार में आई इस गिरावट के कई कारण हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक अर्थशास्त्र के व्यवहार में आई गिरावट है।
अर्थशास्त्र को अकसर एक वैज्ञानिक प्रणाली बताया जाता है। लेकिन वैज्ञानिक निष्कर्ष भी हमारे मूल्यों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं और वैज्ञानिक निष्पक्षता के दावों का इस्तेमाल हमारी नैतिक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्यों को जायज ठहराने के लिए किया जा सकता है।
वास्तव में, मुख्यधारा के अर्थशास्त्र- विशेष रूप से लंबे समय से प्रचलित नव-उदारवादी विचारधारा, जो विकास, दक्षता, मुक्त बाजार पर जोर देती है- ने लालच, शोषण और विषमता को न केवल उचित ठहराया है, बल्कि प्रोत्साहित भी किया है।
नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के ‘कैपेबिलिटी एप्रोच’ पर आधारित 2012 के एक अध्ययन में पाया गया था कि शिक्षा लोगों को अधिक केयरिंग और मददगार बनाने में मदद करती है, लेकिन जिस तरह से अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, यह स्वार्थ को एक सामान्य या वांछनीय नैतिक सिद्धांत के रूप में बढ़ावा दे सकता है।
एक अन्य नोबेल विजेता अर्थशास्त्री केनेथ एरो ने कहा था, बाजार तब तक काम नहीं कर सकते, जब तक प्रतिस्पर्धी फर्म और व्यक्ति भी अपने पारस्परिक दायित्वों का सम्मान न करें। दूसरे शब्दों में, वे विश्वास और सहयोग पर निर्भर हैं। एरो ने मुख्यधारा के अर्थशास्त्र की उस प्रवृत्ति को भी चुनौती दी, जिसमें स्वतंत्रता और समानता को विरोधाभासी माना जाता है।
नव-उदारवादी तर्क यह है कि किसी भी मात्रा में असमानता स्वाभाविक है और इसे कम करने का कोई भी हस्तक्षेप स्वतंत्रता को नष्ट करता है। लेकिन कई संदर्भों में स्वतंत्रता और समानता लगभग एक जैसी है। समानता को कमजोर करने वाले कार्य- जैसे हड़ताल या आर्थिक दबाव के अधिक सूक्ष्म रूप- श्रमिकों की स्वतंत्रता को भी काफी सीमित करते हैं।
वहीं एक छोटे-से कुलीन वर्ग द्वारा अर्थव्यवस्था का दोहन यह दर्शाता है कि औपचारिक लोकतंत्र और स्वतंत्रता एक छद्म है। अंततः, एरो ने लिखा, जो संस्थाएं घोर असमानताओं को जन्म देती हैं, वे मनुष्यों की समानतापूर्ण गरिमा का अपमान हैं।
दार्शनिक इसाया बर्लिन ने इसका सार प्रस्तुत करते हुए कहा था- भेड़ियों की स्वतंत्रता का अर्थ अकसर भेड़ों की मृत्यु रहा है। यह चेतावनी आज विशेष रूप से दूरदर्शी है, जब न्यस्त स्वार्थों के पास अपने चुने हुए राजनेताओं और उद्देश्यों की ओर आकर्षित करने के लिए अपार संसाधन हैं, साथ ही जनमत को प्रभावित करने के लिए अभूतपूर्व डिजिटल उपकरण भी हैं। जैसा कि एक अन्य नोबेल विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने कहा है, एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत की जगह एक डॉलर, एक वोट ने ले ली है।
लेकिन आर्थिक स्वार्थ तो समस्या का केवल एक पहलू है। उग्र राष्ट्रवाद भी बढ़ती असमानता में योगदान दे रहा है। एक समय था जब राष्ट्र-राज्य आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था थी। प्रगति को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय गौरव की भूमिका होती थी। लेकिन अब सामूहिक लक्ष्यों पर वैश्विक सहयोग का समय है- एक-दूसरे के लिए लाभकारी व्यापार-व्यवस्थाओं से न्यायसंगत और समावेशी जलवायु-कार्रवाई तक। बाजारों की तरह बहुपक्षीय कार्रवाइयां भी परस्पर विश्वास और सहयोग पर निर्भर करती हैं।
आपसी सहयोग में विश्वास को मजबूत करके, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जैसे बहुपक्षीय संगठन दुनिया के देशों को अपने बलबूते हासिल की जा सकने वाली उपलब्धियों से कहीं ज्यादा हासिल करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इन जैसी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए हमें अपनी नैतिक दिशा को फिर से जांचना होगा। केवल स्वार्थ पर ध्यान केंद्रित करने को तर्कसंगत मानने या अपनी करुणा को केवल उन लोगों तक सीमित रखने के बजाय- जो हमारे जैसे दिखते, बोलते या प्रार्थना करते हैं- हमें मानवता को अधिक महत्व देना चाहिए।
एक समय था जब राष्ट्र-राज्य आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था थी। प्रगति को बढ़ावा देने में भी राष्ट्रीय गौरव की अहम भूमिका होती थी। लेकिन अब सामूहिक लक्ष्यों पर वैश्विक सहयोग का समय है।
 Date: 17-10-25
Date: 17-10-25
जलवायु परिवर्तन मोर्चे पर निष्क्रियता का एक दशक
श्याम सरन, ( लेखक विदेश सचिव रह चुके हैं और साल 2007-2010 के दौरान जलवायु परिवतर्न पर भारत के मुख्य वार्ताकार थे )
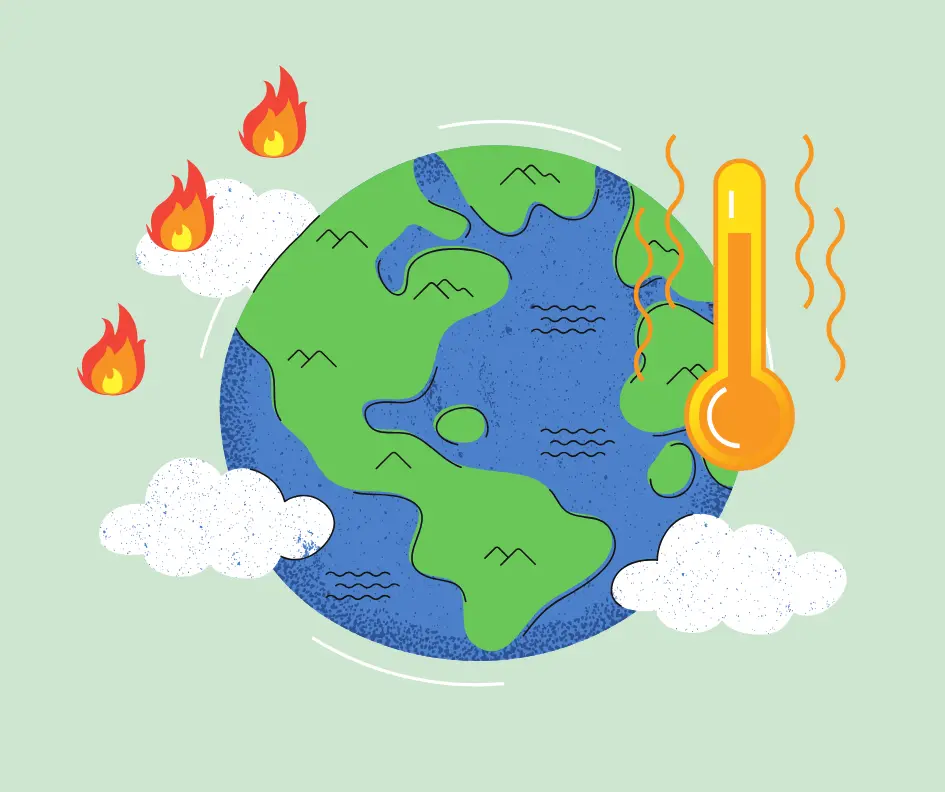
आज से 33 वर्ष पहले 1992 में मैं भी उस भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था जो रियो डी जेनेरियो में अंतिम दौर की वार्ता में शामिल हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के रूप में सामने आया । यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन के आसन्न संकट से निपटने का एक बहुपक्षीय प्रयास था। विकासशील देशों के लिए इसमें कुछ अहम प्रावधान थे।
इनमें से एक था 19वीं सदी में जीवाश्म ईंधन आधारित औद्योगिक दौर की शुरुआत के बाद पृथ्वी के वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित और औद्योगिक देशों की ऐतिहासिक जवाबदेही के सिद्धांत को मान्यता देना ।
कार्बन उत्सर्जन वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है और समय के साथ इसमें बहुत मामूली कमी आती है। मौजूदा उत्सर्जन जिसमें विकासशील देशों का उत्सर्जन भी शामिल है, पहले से मौजूद कार्बन में चरणबद्ध इजाफा करता है। पहले से भंडारित कार्बन और अब वातावरण में उत्सर्जित कार्बन की यह दलील ही जलवायु बहस के केंद्र में है।
दूसरा, यूएनएफसीसीसी ने ‘साझा किंतु भिन्न जिम्मेदारियों और संबद्ध क्षमताओं’ का सिद्धांत दिया जिसे सीबीडीआर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ यह है कि एक ओर जहां ऐतिहासिक कारणों से जलवायु परिवर्तन से निपटना सभी देशों की जिम्मेदारी है वहीं चूंकि विकसित देशों के पास धन तथा तकनीकी संसाधन उपलब्ध हैं इसलिए उन्हें ही इस प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिए। यूएनएफसीसीसी ने यह भी माना कि विकासशील देशों द्वारा जलवायु कार्रवाई, जो वे अपनी सीमित संसाधनों के भीतर नहीं कर सकते, उन्हें विकसित देशों से वित्त और तकनीक दोनों के माध्यम से सहयोग मिलना चाहिए। यह वित्त मुख्य रूप से सार्वजनिक राजस्व से आना था, और तकनीक का हस्तांतरण सरकार से सरकार के स्तर पर किया जाना था। निजी और परोपकारी योगदान इन दोनों का पूरक हो सकते थे, लेकिन वे राज्य स्तरीय कार्रवाई
का विकल्प नहीं बन सकते थे।
ये सिद्धांत और प्रावधान 1997 में अपनाए गए क्योटो प्रोटोकॉल में भी दोहराए गए। प्रोटोकॉल में उत्सर्जन में कमी के लिए दो प्रतिबद्धता अवधि सुझाई गई थीं। पहला 2008 से 2012 तक और दूसरा 2013 से 2020 तक। इसका निर्धारण 2013 में दोहा संशोधन को अपनाने के बाद किया गया। 37 औद्योगिक देशों और यूरोपीय संघ ने आपस में पहले प्रतिबद्धता अवधि के लिए लागू होने वाले उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर बातचीत की। इस चरण के दौरान विकासशील देशों से यह उम्मीद नहीं थी कि वे कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य मानेंगे। यह केवल 2008 से 2012 तक की चार वर्ष की अवधि के लिए था। दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के लिए कुल उत्सर्जन लक्ष्य में कमी का काम बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाए।
क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन कदमों से संबंधित एक अहम उपाय था। इसकी अनुपालन प्रक्रिया बहुत मजबूत थी। अगर कोई देश पहली प्रतिबद्धता अवधि में अपनी उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में कमी नहीं कर पाता तो कमी को न केवल दूसरी प्रतिबद्धता में जोड़ दिया जाता बल्कि अतिरिक्त उत्सर्जन कटौती के रूप में 30 फीसदी जुर्माना भी लगाने की बात कही गई थी।
पहला झटका तब लगा जब अमेरिका ने समझौते का पालन नहीं किया और खुद को समझौते से बंधा हुआ नहीं माना। अमेरिका का यह व्यवहार बाद की वार्ताओं में भी दिखता रहा। इसमें 2015 का पेरिस समझौता भी शामिल है। वर्ष 2007 में आयोजित बाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप) में यूएनएफसीसीसी को बचाने का प्रयास किया गया। इसमें सर्वसम्मति से बाली रोडमैप और बाली एक्शन प्लान को अपनाया गया। इसके दो प्रमुख परिणाम थे पहला, यूएनएफसीसीसी के सिद्धांतों और प्रावधानों के क्रियान्वयन को एक व्यापक प्रक्रिया के जरिये मजबूत करना ताकि इस संधि की पूर्ण, प्रभावी और सतत क्रियान्वयन को संभव बनाया जा सके। इसके लिए दीर्घकालिक सहयोगी कार्रवाई पर एक विशेष कार्य समूह की स्थापना की गई जो 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित 15वें कॉप तक बहुपक्षीय वार्ताओं में लगा रहा। बाली कार्ययोजना चार स्तंभों पर आधारित थी- उत्सर्जन में कमी, अनुकूलन, वित्त और प्रौद्योगिकी। दूसरा, विकासशील देशों के लिए महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बाली कार्य योजना ने उनके द्वारा की जाने वाली जलवायु कार्रवाई और विकसित देशों द्वारा वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करने के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित किया।
तब से अब तक जलवायु गाथा एक निंदात्मक, योजनाबद्ध और अंततः आत्मघाती प्रयास रही है, जिसमें विकसित देशों ने यूएनएफसीसीसी को कमजोर करने एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज यानी क्योटो प्रोटोकॉल से बिना किसी दंड के बाहर निकलने और विकसित व विकासशील देशों के बीच के अंतर को मिटाने की कोशिश की। मैं 2007 से 2010 तक भारत का प्रमुख जलवायु वार्ताकार होने के नाते इसका प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं, और बाद की वार्ताओं का पर्यवेक्षक भी। इन वार्ताओं में हमारे विकसित देश साझेदारों ने क्या हासिल किया?
पहली बात, 2015 तक पेरिस समझौता बैठक में ऐतिहासिक जवाबदेही के सिद्धांत को त्यागा जा चुका था। इसका अर्थ यह भी था कि विकसित और विकासशील देशों के बीच का स्पष्ट भेद समाप्त कर दिया गया था और पूरा ध्यान वर्तमान उत्सर्जन पर केंद्रित कर दिया गया। आने वाले वर्षों में भारत का उत्सर्जन बढ़ना लाजमी है। भले हमारा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का आधा हो ।
दूसरा, उत्सर्जन, वित्त या प्रौद्योगिकी से संबंधित कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं की अवधारणा को त्याग दिया गया है और उसकी जगह स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं को अपनाया गया है। अब ‘वचन और समीक्षा’ प्रणाली लागू है, जिसमें केवल ‘नाम उजागर करना और शर्मिंदा करना’ ही प्रेरक तत्व हैं। हम जानते हैं कि ये कितने प्रभावी होंगे।
वर्ष 2015 का पेरिस जलवायु समझौता यूएनएफसीसीसी को कमजोर करने की इस प्रक्रिया को वैधता प्रदान करता है, जिसमें विकसित देशों की ओर से कमजोर आकांक्षात्मक लक्ष्य और अस्पष्ट प्रतिबद्धताएं शामिल थीं। यह क्षरण प्रक्रिया अब भी जारी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस वर्ष नवंबर में होने वाला कॉप 30 भी इससे अलग नहीं होगा, भले ही मेजबान ब्राजील इसे क्रियान्वयन कॉप कह रहा हो । एक सर्वसम्मत दस्तावेज अपनाने और जीत की घोषणा करने का दबाव एक बार फिर न्यूनतम साझा सहमति वाले परिणाम को सुनिश्चित करेगा।
यह अफसोस की बात है कि भारत ने, वास्तव में, अपने और अन्य विकासशील देशों के हितों को नुकसान पहुंचाते हुए, इस क्षय प्रक्रिया को चुपचाप स्वीकार कर लिया है। अभी भी देर नहीं हुई है कि हम सच्चाई को स्वीकार करें और उन लोगों का सामना करें जो अपने ही महत्त्वपूर्ण हितों की निंदात्मक उपेक्षा के माध्यम से पृथ्वी को खतरे में डाल रहे हैं। यह एक वैश्विक चुनौती है और कोई भी देश उस खतरे से नहीं बच पाएगा जो हमारी सामूहिक उदासीनता से उत्पन्न होगा। चेतावनी के संकेत पहले से ही मौजूद हैं।
आभासी दुनिया के वास्तविक जोखिम
सुनील कुमार
पिछले कुछ वर्षों से यह साफ देखा जा सकता है कि स्मार्टफोन का किस स्तर पर विस्तार हुआ है और युवाओं के बीच इसका उपयोग किस कदर बढ़ गया है ऐसे उदाहरण आसानी से मिल जाएंगे, जिसमें युवा पढ़ाई और किसी नियमित रोजगार का मार्ग चुनने के बजाय ‘रील’ बना कर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर उससे कमाई के रास्ते तलाश रहे हैं। यह अब लाखों युवाओं की हकीकत बन चुकी है। आज सोशल मीडिया के इस दौर में ‘रील’ केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि यह पैसा और शोहरत कमाने का माध्यम बन चुका है। यह मानसिकता पढ़े-लिखे युवाओं से लेकर आम गृहिणियों, कामकाजी महिलाओं और ट्रक चालकों से लेकर घर-घर सामान पहुंचाने वालों तक फैल चुकी है। कभी मनोरंजन के लिए शुरू हुई यह डिजिटल संस्कृति अब युवाओं के जीवन में वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच की सीमाओं को धुंधला कर रही है। गांव, शहर, कस्बा और महानगर हर जगह युवा कैमरे के सामने अभिनय करते, सड़कों पर नाचते या खतरनाक करतब करते दिखाई देते हैं। इस क्रम में वे अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूकते हैं।
पहले युवा वर्ग डाक्टर इंजीनियर, अधिकारी, लेखक, सैनिक या खिलाड़ी आदि बनने का सपना देखता था। कुछ युवा फिल्मों से प्रभावित होकर अभिनय की दुनिया में कदम रखने के लिए वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद अपना स्थान मुश्किल से बना पाते थे। मगर आज का युवा परिश्रम के बजाय ‘इन्फ्लुएंसर’ (समाज में अपना प्रभाव बनाने वाला) बनना चाहता है। अब लक्ष्य ज्ञान या कौशल नहीं, बल्कि लोकप्रियता हासिल करना और थोड़े समय में दौलतमंद बन जाना है। यह संस्कृति एक नई मानसिकता को जन्म दे रही है, जो सामाजिक विकृति का कारण भी बन रही है। ‘रील’ बनाना अब कला नहीं, बल्कि एक प्रतिस्पर्धा है।
समाज में सहयोग की जगह तुलना और प्रतियोगिता ने ले ली है, जहां हर कोई दूसरों से अधिक लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कोई चलती ट्रेन के पास नृत्य करता है, कोई पुल से कूदता है, कोई सड़क पर करतब दिखाता है, तो कोई सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर रख कर सोशल मीडिया के लिए सामग्री तैयार करता है। इससे कई तरह की मानसिक और सामाजिक विकृतियां भी पैदा हो रही हैं, जो कई बार हत्या या आत्महत्या जैसी आपराधिक घटनाओं के रूप में सामने आती है। युवा सोचते हैं कि यदि उन्होंने कुछ अनोखा किया, चाहे उसमें जान का जोखिम क्यों न हो, उससे उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी। मगर कई बार इसकी कीमत जान गंवा कर चुकानी पड़ती है।
देश में रेल मार्ग के पास इस तरह के वीडियो बनाते हुए कितने लोगों की जान जा चुकी है, इसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। मगर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और नागपुर मंडल के एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2025 के शुरुआती पांच महीनों में सत्तानबे लोग ट्रेन से कट कर मारे गए, जो ‘रील’ बनाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका की ‘बार्बर ला फर्म’ की रपट के अनुसार, दुनिया भर में सेल्फी लेते समय मौत की घटनाओं में से
42.1 फीसद घटनाएं भारत में हुई हैं। ये महज हादसे नहीं, बल्कि उस समाज की त्रासदी है, जिसने वास्तविक जीवन के बजाय आभासी छवि को – अधिक मूल्यवान बना दिया है। युवाओं में बढ़ती यह प्रवृत्ति उन्हें वास्तविक संवाद, पढ़ाई, संबंध और सामाजिक जिम्मेदारी से दूर ले जा रही है।
इस संस्कृति का एक और खतरनाक पहलू अभद्रता और हिंसा का महिमामंडन है। आज सोशल मीडिया पर मौजूद अधिकांश सामग्री सामाजिक शालीनता की सीमाओं को लांघ चुकी है। विडंबना यह है कि इस तरह की सामग्री को दर्शक भी पसंद करने लगे हैं। किसी समाज की सभ्यता का आकलन इस बात से भी किया जाता है कि वह अपने युवाओं को किस दिशा में प्रेरित करता है। जब युवाओं की ऊर्जा ऐसी सामग्री तैयार करने में लग रही है, तो यह सामाजिक पतन का स्पष्ट संकेत है। आज कोई यह नहीं पूछता कि हमारी शिक्षा और पारिवारिक व्यवस्था इतनी असफल क्यों हो गई कि युवा अपनी पहचान सिर्फ कैमरे में खोजने लगा है।
आभासी दुनिया से जुड़ी इस संस्कृति ने न केवल युवाओं की ऊर्जा को भटकाया है, बल्कि समाज की नैतिकता को भी चोट पहुंचाई है। सड़क दुर्घटनाओं के दौरान मदद करने के बजाय लोग अब मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इस तरह की सामग्री के प्रसार का लोभ मानवता से बड़ा हो गया है। अब मानवीय संवेदनाओं की जगह प्रसिद्धि का आकर्षण साफ दिखाई देता है। बच्चों के साथ माता-पिता के संवाद और मित्रता का स्थान अब स्क्रीन ने ले लिया है। यही कारण है कि मोबाइल बच्चों का शिक्षक, मित्र और आदर्श बनता जा रहा है। दुखद यह है कि इस बदलती मानसिकता के बीच परिवार, शिक्षक और समाज मौन हैं। समाचार माध्यम भी सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने वाली सामग्री को खबर के रूप में परोसते हैं, जिससे युवाओं के बीच इस तरह की सामग्री बनाने की होड़ और तेज हो जाती है।
वीडियो के जरिए ‘रील’ की फलती-फूलती संस्कृति सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि आर्थिक तंत्र का हिस्सा भी है। लोग सोशल मीडिया पर सामग्री डाल कर पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए वे वही सामग्री आगे बढ़ाते हैं, जो अधिक लोगों को आकर्षित करे, चाहे वह कितना भी सतही, हिंसक या अपमानजनक या अभद्र क्यों न हो। युवाओं को शायद ही इस बात का एहसास होता है कि वे डिजिटल उत्पाद बनते जा रहे हैं। उनका समय, ध्यान और भावनाएं डेटा तथा विज्ञापन के रूप में बिक रहे हैं। युवा सोचते हैं कि वे रचनाकार हैं, जबकि वास्तव में वे एक उपभोक्ता हैं, जिन्हें बार-बार स्क्रीन पर आने के लिए आकर्षित किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर ‘रील’ का जुनून केवल व्यक्ति का बाहरी व्यवहार नहीं बदलता, बल्कि उसके भीतर की दुनिया को भी विकृत कर देता है। अब सफलता की दर प्रसिद्धि और समर्थकों की संख्या से मापी जाने लगी है। यही तत्त्व दोस्ती, प्रेम और आत्मविश्वास का पैमाना बन गए हैं। मनोचिकित्सक मानते हैं कि ‘डोपामिन हिट’ यानी ‘रील’ को पसंद करने वालों की संख्या से मिलने वाली क्षणिक खुशी अब डिजिटल नशे का रूप ले चुकी है। युवा इस भ्रम को हकीकत मानने लगे हैं कि सोशल मीडिया पर सराहना ही उनकी असली पहचान है। इस प्रवृत्ति के कारण वे वास्तविक जीवन से कटने लगे हैं, पढ़ाई और अपने कार्य में उदासीन हो गए हैं तथा मानसिक अस्थिरता का शिकार होने लगे हैं। युवाओं को यह समझना होगा कि असली पहचान स्क्रीन पर नहीं, वास्तविक जीवन में है जितना वे अपनी प्रतिभा और संवेदनशीलता को वास्तविक समाज में लगाएंगे, उतना ही उनका अस्तित्व अर्थपूर्ण बनेगा। जरूरत है आज की युवा पीढ़ी को सही दिशा देने की, ताकि कैमरे के सामने सिर्फ दिखावे के बजाय विचार, संवेदना और परिवर्तन की सच्ची तस्वीर बने ।
प्रशासन में जाति-भेद
संपादकीय
प्रशासन से जुड़ी कुछ ऐसी गंभीर शिकायतें सामने आई हैं, जिनसे पता चलता है कि प्रशासनिक अधिकारियों के बीच आंतरिक रूप से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या और उसके बाद सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) संदीप लाठर की मौत ने न केवल हरियाणा, बल्कि देश भर में लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। देश के आला अधिकारी इस पर क्या सोचते हैं, यह तो स्पष्ट नहीं है, मगर लोगों को यह तो पता चल ही गया है कि उच्चाधिकारियों के बीच संवाद, समन्वय, परस्पर सम्मान का स्तर ऊंचा नहीं है। आईपीएस पूरन की कथित आत्महत्या का मामला जातिभेद से लेकर भ्रष्टाचार और अपराध की दुनिया तक से जुड़ता लग रहा है। इस मामले में रोज कोई नया पहलू जुड़ रहा है। स्वाभाविक ढंग से देखें, तो आत्महत्या करने वाले अधिकारी काफी वरिष्ठ थे। वह 24 साल से आईपीएस थे, क्या उन्होंने जातिगत भेदभाव को इतने वर्षों तक झेला ? आला अधिकारियों पर तो यह जिम्मेदारी होती है कि कमजोर दलितों-पिछड़ों को किसी भी तरह के भेदभाव से बचाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दें। अब तो यह सवाल खड़ा हो गया है कि प्रशासनिक सेवाओं में जातिगत भेदभाव इतना प्रबल है कि आला अधिकारी भी घुटने टेक रहे हैं।
आशंका यह भी जताई जा सकती है कि हरियाणा का यह मामला अकेला नहीं है, तो क्या प्रशासनिक प्रशिक्षण के दौरान ही जातिगत भेदभाव जैसी खराबी को दूर नहीं किया जा रहा है? एक आईपीएस की कथित आत्महत्या पूरी प्रशासनिक सेवा के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। यह आईपीएस अधिकारी अपने अंतिम संदेश में एक नहीं, बल्कि आठ वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगा गए हैं। अब इन आठ अधिकारियों का क्या होगा ? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उनके अपराध को उनका महकमा कैसे प्रमाणित करेगा ? अगर प्रशासन में जातिगत भेदभाव है, तो क्या जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं होगी ? भूलना नहीं चाहिए, इन आईपीएस अधिकारी की पत्नी वरिष्ठ आईएसएस अधिकारी हैं और प्रारंभ में उनका जो व्यवहार रहा, उससे यही संदेश गया है कि एक प्रशासनिक अधिकारी का भी अपने प्रशासन पर विश्वास पुख्ता नहीं है। अपने आईपीएस पति के शव का पोस्टमॉर्टम रोकने का जो प्रयास आईएसएस पत्नी ने किया, उससे कुछ देर में ही कई सवाल खड़े हो गए। हालांकि, उन्होंने बाद में प्रशासन पर पूरा विश्वास जताया, मगर इससे पहले जो कुछ हुआ, वह प्रशासन की कमियों में शुमार हो गया। एक बड़ा सवाल भ्रष्टाचार का है? इसी मामले में भ्रष्टाचार के ताजा आरोप भी कहीं बाहर से नहीं लगे हैं, बल्कि एक ऐसे एएसआई ने लगाए हैं, जो खुद जांच में शामिल थे और जिन्होंने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। अब क्या होना चाहिए? यहां पति को खोने वाली आईएएस अधिकारी की गुहार पर ध्यान देना चाहिए कि ‘मुझे पूरी उम्मीद है, जांच पेशेवर, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से की जाएगी, ताकि कानून के अनुसार सच्चाई सामने आए। वाकई, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। समग्रता में देखें, तो अगर देश में प्रशासनिक सुधार की जरूरत है, तो इस कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। गौर कीजिए, गुरुवार को ही पंजाब के एक डीआईजी को सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन से शिकायत की लंबी होती सूची का एक ही इशारा है कि खेत को बाड़ से बचाने की जरूरत आन पड़ी है।
Date: 17-10-25
हेलसिंकी से यातायात प्रबंधन सीखें हमारे महानगर
प्रवीण कौशल, ( तकनीक और सामाजिक उद्यमी )
दीपावली के दिन करीब आते ही सड़क मार्ग से दिल्ली- गुरुग्राम की दैनिक यात्रा करने वाले लाखों लोगों की चिंताएं गहराने लगी हैं। वजह? भयानक ट्रैफिक ! यूं भी हर सुबह गुरुग्राम एक धीमी गति वाले अव्यवस्थित नाटक में बदल जाता है। हॉर्न की आवाजें, धुएं के बादल और झुंझलाहट- ये सब मिलकर एक ऐसे चक्र का निर्माण करते हैं, जिसे हमने सामान्य जीवन मान लिया है। दस किलोमीटर की दूरी तय करने में दो-दो घंटे लगना, आसमान छूता मानसिक तनाव और गिरती उत्पादकता, मगर जवाबदेही किसी की नहीं।
अगर हम इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में देखते, तो शायद कुछ कार्रवाई करते । रोजाना का जाम केवल असुविधा नहीं है, यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी नुकसानदेह है। मगर सरकारें और समाज, दोनों ने इसे ‘न्यूनॉर्मल’ के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए इस संकट की अनदेखी की जाती है। हालांकि, इस समस्या का समाधान निकालने का विज्ञान हमारे पास है, मगर हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं! भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक गणितीय मॉडल विकसित किया है, जिससे ट्रैफिक नियंत्रण एल्गोरिदम को कुशलता से परखा जा सकता है। यह मॉडल ‘टू- बिन नेटवर्क मॉडल’ कहलाता है। एक सरल, पर प्रभावशाली तरीका, जिससे वाहन प्रवाह को समझा और अनुकूलित किया जा सकता है। हर गाड़ी को ‘सिमुलेट’ करने के बजाय यह मॉडल सड़कों को दो मुख्य दिशाओं में बांटता है और उनके बीच वाहनों के प्रवाह का विश्लेषण करता है। इससे कम कंप्यूटिंग संसाधनों में ही यह समझा जा सकता है कि कौन सी नीति जाम को जल्दी व बेहतर तरीके से खत्म कर सकती है।
हमारे महानगरों को ऐसी डाटा आधारित वैज्ञानिक प्रणाली की बेहद जरूरत है। हरेक नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर शहर का सटीक ट्रैफिक मॉडल तैयार करना चाहिए। अब अनुभव के आधार पर ट्रैफिक नहीं संभाला जा सकता; इसे मापना और संचालित करना ही होगा। गुरुग्राम का उदाहरण सामने है। यहां ढांचा है, लेकिन प्रणालीगत डिजाइन नहीं है। लिहाजा आए दिन जाम की समस्या पैदा होती रहती है। समस्या यह है कि नगर निगम, जीएमडीए, एनएचएआई, हुडा और ट्रैफिक पुलिस, सभी की जिम्मेदारी एक-दूसरे से टकराती है। एक ट्रैफिक सिग्नल खराब हो जाए, तो कोई नहीं जानता कि उसे ठीक कौन करेगा ? जाम की कई वजहें हैं। पहली वजह तो यही है कि हर मध्यवर्गीय व्यक्ति का सपना एसयूवी है, सार्वजनिक परिवहन नहीं। दरअसल, हमारे यहां सार्वजनिक परिवहन की हालत बेहद खराब है। फिर हमारे शहरों में बिना सुचिंतित योजना के सड़कें चौड़ी कर दी जाती हैं। उन पर सिग्नल समन्वय, जल निकासी व फुटपाथ की अहमियत ही नहीं समझी जाती। फ्लाईओवर एक जाम हल करता है, तो दूसरा जाम 500 मीटर आगे बढ़ जाता है।
हमारे महानगर हेलसिंकी से सबक ले सकते हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी ने साल 2024 में शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। ऐसा किसी संयोग से नहीं हुआ, बल्कि यह सुनियोजित सुधारों का परिणाम था। नगर प्रशासन ने वहां गति सीमा में कमी की। आधे से अधिक इलाकों में गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई, जिससे दुर्घटनाओं की तीव्रता और संख्या, दोनों घट गई। ऊंचे-ऊंचे क्रॉसवॉक, सुरक्षित चौराहों और बेहतर प्रकाश व्यवस्था ने पैदल यात्रियों व साइकिल सवारों की रक्षा की । सार्वजनिक परिवहन, साइकिल लेन और पैदल चलने की सुविधाओं में भारी निवेश किया गया। इससे निजी कारों पर निर्भरता घटी। सख्त ट्रैफिक पुलिसिंग से एक सुरक्षित ड्राइविंग संस्कृति बनी।
जाम की समस्या से जूझने वाले हमारे तमाम शहरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित सिग्नल सिस्टम परीक्षण के लिए आईआईटी बॉम्बे का ‘टू-बिन मॉडल’ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेन अनुशासन और नो पार्किंग जोन का पालन सख्ती से हो। जब तक इस तरह के कदम नहीं उठाए जाएंगे, ट्रैफिक समस्या सिरदर्द बनी रहेगी।
