
24-09-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 24-09-25
Right to state
Recognition of Palestine is more than Just symbolic
Editorials
When the state of Israel was declared in Palestine on May 14, 1948, the U.S. recognised it in just 11 minutes. In the years since, most UN members extended recognition to the Jewish nation, which became a UN member in 1949. When the Palestine Liberation Organisation (PLO) declared a state of Palestine in 1988, much of the Global South recognised it, but powerful western nations stayed away with the position that recognition would come only as part of a negotiated two-state settlement. But this week, at the UN General Assembly, the U.K., France, Canada and Australia finally recognised Palestine, which shows their fraying ties with Israel and diminishing faith in a coercion-free diplomatic process leading to a final settlement. For Palestinians, the western recognition could be seen as a diplomatic respite but comes too late -Gaza has been devastated by Israeli forces; Jewish settlements and Israeli checkpoints have mushroomed in the West Bank; and settler violence has displaced thousands of Palestinians over the past two years. Israel’s Prime Minister Ben- jamin Netanyahu openly declares that there will never be a Palestinian state, and Washington offers Israel unconditional support.
Recognition may not have an immediate impact on the ground. Israel’s ruling coalition is incapable of even ending the slaughter in Gaza, let alone discuss a two-state solution. Yet, this wave of recognition is not just a symbolic act. It shows cracks in the post-1948 pro-Israel consensus in the West. The U.K. played a decisive role in the establishment of the state of Israel. France armed it in its early years and helped it build nuclear weapons. These powers bear historical responsibility to find a solution to the problem they were a party to from the beginning. And Palestinians have an internationally recognised right to have their own independent, sovereign state. If Israel does not stop the war in Gaza, which should be the first step, and continues with the settlements in the West Bank, Europe should impose an arms embargo on Tel Aviv. Israel should be warned against annexing the West Bank, which should be treated as a red line. Mr. Netanyahu and his extremist Ministers, though internationally isolated, will not be persuaded. But they will not rule forever. A future Israeli leader could abandon Mr. Netanyahu’s militarism. This forever war and genocidal tag are not helping Israel’s interests either, even though it allows Mr. Netanyahu to cling on to power. The recognition of today should serve as a stepping stone for a Palestinian state tomorrow. That is the best chance for peace for Palestinians, Israelis and West Asia.
Date: 24-09-25
हम अपने टेक-टैलेंट्स को पहचानकर आगे बढ़ाएं
संपादकीय
ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे शोधों की गुणवत्ता को 6 इंडिकेटर्स पर परखने वाली ताजा स्टैनफर्ड एल्सीवियर रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में हुए विश्व स्तरीय और उच्च गुणवत्ता के शोधों में से 42% का विषय इंजीनियरिंग, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलोजी और आईटी है, जबकि प्योर साइंस (फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स) और हेल्थ साइंस का हिस्सा क्रमशः 27 और 21% है। इसके उलट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शोध ( 38% ) हेल्थ साइंस में हुए, जबकि टेक- संबंधित तीनों विषयों और प्योर साइंस का शेयर मात्र 23 और 19% रहा। जहां भारत का वैश्विक उच्च गुणवत्ता शोध में औसत हिस्सा 2.4% रहा, वहीं टेक-संबंधी और प्योर साइंस के शोध में यह बढ़कर क्रमशः 13 और 10% हो गया । यह युग शुद्ध टेक – ज्ञान का है और दौर एआई से आगे बढ़ते हुए क्वांटम कम्प्यूटिंग का । इसमें पीछे रहने वाला समाज हर आयाम पर पिछड़ेगा। भले ही दुनिया की आबादी का 17.5% शेयर रखने वाला भारत शोध की दौड़ में मात्र 2.4% पहचान बना सके, चिंताजनक है। लेकिन टेक विषयों पर 13% हिस्सा गर्व का अहसास है। यह तब है जब भारत अपनी जीडीपी का 0.6% ही शोध पर खर्च करता है। एक जमाने में भारत के शोधों के मुख्य विषय दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्य और लिबरल आर्ट्स होते थे, लेकिन आज उनका वैश्विक स्तर पर शेयर मात्र 0.3% रह गया है । अर्थशास्त्र और प्रबंधन का शेयर भी महज 1.7% है। रिपोर्ट के नतीजों के परिप्रेक्ष्य में सरकार को अपनी नीति बदलनी होगी।
Date: 24-09-25
मैन्युफैक्चरिंग को घटाकर विकास नहीं बढ़ा सकते हैं
रुचिर शर्मा, ( ग्लोबल इन्वेस्टर व लेखक )
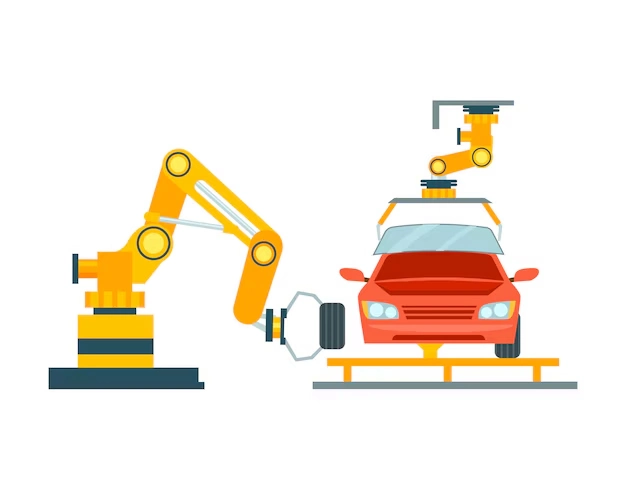
जकार्ता में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों ने एक आर्थिक सितारे के आसमान से गिरने के कारणों पर सवाल खड़े किए हैं। यह सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं। दक्षिण-पूर्वं एशिया जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस वियतनाम शामिल हैं- कई लुप्त होते सितारों का क्षेत्र है। कभी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का केंद्र रहा यह क्षेत्र हाल में आर्थिक विकास की तेजी से घटती उम्मीदों का घर बन गया है। 2010 के बाद दशक में दक्षिण-पूर्व एशिया के शेयर बाजारों ने उभरते हुए देशों के किसी भी क्षेत्र की तुलना में सबसे अच्छा रिटर्न दिया था। लेकिन पिछले एक साल में किसी भी क्षेत्र की तुलना में इनका रिटर्न सबसे खराब रहा है।
पश्चिम के साथ भू-राजनीतिक तनाव ज्यादा दखल देने वाली हुकूमत और बढ़ती लागतों के डर से जैसे-जैसे वैश्विक निर्माताओं ने चीन से उत्पादन हटाना शुरू किए थे, दक्षिण-पूर्व एशिया को इससे सबसे ज्यादा फायदा होने की सम्भावना दिख रही थी। इस क्षेत्र के कई देशों के पास पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत आधार था, जिस पर वे आगे बढ़ सकते थे। लेकिन निवेश में बदलाव पर कोई खास असर नहीं दिखा। इसके बजाय, चीन ने अपने सरप्लस उत्पादन का निर्यात दक्षिण-पूर्व एशिया में करना शुरू कर दिया- किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में ज्यादा जिससे इन देशों के लिए अपने घरेलू बाजारों में भी हिस्सेदारी बनाए रखना मुश्किल हो गया।
दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में सबसे लचीला वियतनाम रहा है। चीन की डंपिंग और अमेरिकी टैरिफ के दबाव का मुकाबला करने के लिए इसने निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने और सरकारी कम्पनियों को सुव्यवस्थित करने के लिए घरेलू सुधारों को आगे बढ़ाया। इसके बाद मलेशिया का नंबर आता है, जिसने अपने फायदों को बढ़ाने के लिए खासकर डेटा सेंटरों के क्षेत्र में कुछ कदम जरूर उठाए। इस बीच राजनीतिक उथल-पुथल में फंसे थाईलैंड ने अपने स्थिर मैन्युफैक्चरिंग – बेस को बचाने के लिए कुछ खास नहीं किया है। और इंडोनेशिया अपने नए राष्ट्रपति प्रबोवो के नेतृत्व में सच्चाई से मुंह फेरने की स्थिति में चला गया है। ऐसे में क्या आश्चर्य कि जिस देश ने हालात का बेहतर सामना किया, उसने सबसे अच्छे नतीजे भी दिए । वियतनाम एकमात्र दक्षिण-पूर्व एशियाई शेयर बाजार है, जो अभी भी मजबूत रिटर्न दे रहा है; वहीं इंडोनेशिया का शेयर बाजार सबसे ज्यादा गिरा है।
चीन के कारण इस पूरे क्षेत्र – खासकर इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चरिंग कमजोर हो रही है, जिससे शहरी मजदूर फिर से ग्रामीण इलाकों की ओर लौट रहे हैं। खपत कमजोर हो रही है। पिछले दशक में कारों की बिक्री में तेजी से गिरावट आई है और अब यह मलेशिया- जिसकी आबादी इंडोनेशिया के आठवें हिस्से के बराबर है- से भी कम है। निवेश और निर्माण क्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, इसलिए सीमेंट की बिक्री गिर रही है। प्रबोवो द्वारा उठाए कदम हालात को और बदतर बना रहे हैं।
वे इंडोनेशिया की विकास दर को 8 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात करते हैं। एशियाई निर्यात चमत्कारों के अलावा किसी अर्थव्यवस्था ने शायद ही इतनी विकास दर को कभी बनाए रखा हो, और 2000 के दशक के बाद से तो ऐसा किसी भी देश ने नहीं किया। अच्छी नौकरियां पैदा करने के लिए निवेश करने के बजाय उन्होंने कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है, जिसमें आत्मनिर्भर ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए समर्थन भी शामिल है। यह औद्योगीकरण-विरोधी ट्रेंड्स को और बढ़ावा देगा |
18वीं सदी की कृषि संबंधी रूमानियत की यह अंतर्निहित भावना एक ऐसे नेता की छवि को पुष्ट करती है, जिसका यथार्थ से संपर्क कटता जा रहा है। हाल ही की अपनी जकार्ता यात्रा के दौरान अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि प्रबोवो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, जो उन्हें वही बताते हैं, जो वे सुनना चाहते हैं।
Date: 24-09-25
भारत की चिंता बढ़ाने वाला समझौता
हर्ष वी. पंत, ( लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मैं उपाध्यक्ष हैं )
खुद को एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न मुस्लिम राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने वाले पाकिस्तान ने गत 17 सितंबर को सऊदी अरब के साथ एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते यानी एसडीएमए पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू इसकी वह प्रतिबद्धता है कि किसी भी देश पर हुआ हमला दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। इस समझौते की प्रकृति को देखा जाए तो यह नाटो जैसा सामरिक गठबंधन है। माना जा रहा है कि खाड़ी देशों के लिए सुरक्षा से जुड़े जोखिम और इजरायल के खतरे ने सऊदी अरब को इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया तो पाकिस्तान का ऐसा कोई भी सोच हमेशा भारत केंद्रित होता है। आपरेशन सिंदूर के बाद वह अपने समीकरण नए सिरे से तय करने में जुटा है और यह समझौता भी उसी रणनीति का हिस्सा लगता है। चूंकि बीते कुछ अर्से से भारत ने सऊदी अरब के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में काफी कुछ निवेश किया है, इसलिए इस समझौते के निहितार्थी को समझना आवश्यक है।
सऊदी – पाकिस्तान के संबंधों की जड़ें बहुत गहरी और पुरानी हैं। यहां तक कि पाकिस्तान निर्माण के पहले से ही सऊदी अरब ने एक तरह से उसका समर्थन शुरू कर दिया था। प्रिंस फैसल ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर मुस्लिम लीग की पाकिस्तान परियोजना की पैरवी की थी। सऊदी अरब पाकिस्तान को संप्रभु देश की मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक था। सऊदी अरब के प्रिंस सुलतान ने तो 1960 के दौरान यह तक कहा कि पाकिस्तान हमारा सबसे परम मित्र है और हमें जब भी सैन्य मदद की आवश्यकता होती है तो उस पर ही सबसे अधिक भरोसा रहता है। दोनों देशों के सामरिक रिश्तों में इजरायल भी एक पहलू रहा है। उनके बीच पहले औपचारिक रक्षा समझौते की बात करें तो यह 1967 में हुआ । इसमें पाकिस्तान के सैन्य सलाहकारों ने सऊदी सशस्त्र बलों के विस्तार और आधुनिकीकरण में मदद की। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मिली इस मदद का मोल भारत के खिलाफ युद्धों में पाकिस्तान को समर्थन के रूप में चुकाया ।
भारत के लिए महत्वपूर्ण कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहा। 1965 के युद्ध के दौरान सऊदी ने पाकिस्तान को न केवल विभिन्न प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध कराईं, बल्कि कूटनीतिक आड़ और हरसंभव सहयोग दिया। 1971 के युद्ध और बांग्लादेश संकट के दौरान भी उसका यही रवैया दिखा। उस दौरान सऊदी राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की कार्रवाइयों को निशाना बनाते हुए कहा था कि पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप यूएन चार्टर का उल्लंघन होगा। बांग्लादेश निर्माण के बाद भी सऊदी ने उसे मान्यता देने में हिचक ही दिखाई और पाकिस्तान के रुख की प्रतीक्षा करता रहा। कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बावजूद सऊदी मौन रहा और उलटे भारत पर शांतिपूर्ण समाधान के लिए दबाव बनाता रहा। हालांकि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के समय जरूर सऊदी अरब ने कुछ तटस्थ रुख अपनाया। इसमें भारत की बढ़ते आर्थिक कद की भी भूमिका रही जिसका लाभ सऊदी भी उठा रहा है।
पाकिस्तान के लिए तो सऊदी के साथ हुआ हालिया समझौता ‘अंधे के हाथ बटेर लगने’ जैसा है। बेहद मुश्किल आर्थिक हालात से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी से मिलने वाली वित्तीय सहायता बड़ी राहत देगी। मुस्लिम जगत से जुड़े भू-राजनीतिक ढांचे में भी वह अपना कद बढ़ाने के प्रयास करेगा । इसके अलावा अपने सदाबहार दौस्त चीन और खाड़ी देशों के बीच बिचौलिये की भूमिका में भी काम करता हुआ दिख सकता है। हालांकि इस समझौते में कई बिंदु स्पष्ट नहीं हैं। जैसे क्या सऊदी को पाकिस्तान के परमाणु कवच का भी सहारा मिलेगा? इसकी न तो पुष्टि की गई हैं और न ही खंडन । संभव है कि इसके पीछे अपना खुद का बम बनाने की सऊदी महत्वाकांक्षाओं का भी पेच जुड़ा हो ताकि वह क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़े। सऊदी अरब के लिहाज से यह एकदम स्पष्ट है कि उसकी मंशा ईरान और इजरायल के खिलाफ अपनी ढाल और मजबूत करना है। वहीं पाकिस्तान भारत की बढ़ती शक्ति और प्रभाव की काट चाहता है। इससे ऐसी आशंका बढ़ जाती है कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ किसी संघर्ष में भारत को खाड़ी देशों को लेकर और सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऐसे टकराव में उनकी भूमिका कुछ बढ़ी हुई दिख सकती है। इस समझौते पर अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया में भारत ने यही कहा है कि उम्मीद है कि सऊदी अरब भारत की संवेदनाओं को समझेगा। भारत ने यह भी दोहराया कि राष्ट्रीय हित और सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है, जिसके साथ कोई समझौता नहीं।
इसमें कोई संदेह नहीं कि बीते कुछ समय से भारत ने सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ ही बहुत समय एवं ऊर्जा भी निवेश की है। इन प्रयासों में 2014 में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित सहमति भी शामिल है। इसके बावजूद बदलते भू-राजनीतिक परिवेश को देखते हुए भारत के समक्ष कुछ बाधाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत के सऊदी अरब, ईरान और इजरायल, तीनों के साथ रणनीतिक संबंध हैं। जबकि ये तीनों एक दूसरे के साथ टकराव की स्थिति में हैं और अपना वर्चस्व स्थापित करने में जुटे हैं। इस परिदृश्य में सऊदी अरब – पाकिस्तान रक्षा समझौते ने दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीच भू-राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक दिशा निर्धारित की है । आपसी एकजुटता के संकेत के अलावा, भारत को इस साझेदारी में संभावित सहयोग की सीमाओं और विस्तार का भी सावधानीपूर्वक आकलन करना होगा, ताकि वह अपनी भावी दिशा निर्धारित कर सके। नई दिल्ली के लिए एक बड़ा कार्य सऊदी अरब और पश्चिम एशिया में अन्य भागीदारों के बीच अपने हितों के संतुलन एवं उन्हें साधने की होगी । यह भारतीय विदेश और सुरक्षा नीति के लिए एक प्रमुख चुनौती बनी रहेगी, जिसके मूल में कुछ संभावित व्यापारिक समझौते भी शामिल होंगे।

Date: 24-09-25
लोकतंत्र के लिए नियामकीय संस्थाओं की स्वायत्तता अहम
केपी कृष्णन, ( लेखक आईसीपीपी में मानद सीनियर फेलो और पूर्व अफसरशाह हैं )
अमेरिका से आई हाल की खबरों के मुताबिक, राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त करने की कोशिश की यह एक अभूतपूर्व कदम है जिसके कारण कुक ने पद छोड़ने से इनकार करते हुए ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। फेडरल अपील अदालत ने ट्रंप के खिलाफ आदेश भी दिया। कानून के मुताबिक राष्ट्रपति किसी गवर्नर को सिर्फ ‘कारण बताकर’ ही हटा सकते हैं। ट्रंप के न्याय विभाग ने इससे पहले उनके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की थी और ट्रंप का दावा है कि उन्हें बर्खास्त करने के लिए यह पर्याप्त आधार है।
यह घटनाक्रम लोकतंत्र में शासन के एक मूलभूत सिद्धांत की याद दिलाता है जो शक्तियों के विभाजन और उसके दूसरे पहलू, नियंत्रण और संतुलन से जुड़ा है। हालांकि, यह घटनाक्रम भले ही पूरी तरह अमेरिका से जुड़ा हुआ है लेकिन इससे जो बहस छिड़ती है, उसका ताल्लुक लोकतांत्रिक जवाबदेही बनाम संस्थागत स्वायत्तता से है और यह भारत में भी उतना ही प्रासंगिक है।
यह धारणा कि ‘लोकतांत्रिक जवाबदेही वास्तव में कार्यपालिका को ऐसी निरंकुश शक्ति देती है, न केवल गलत है बल्कि यह शासन की आधुनिक संरचनाओं की अपर्याप्त समझ को भी दर्शाती है। सत्ता से जुड़ी आधुनिक संरचनाओं को देखने से पहले, यह जानना जरूरी है कि भारत में हमने एक ऐसा संवैधानिक ढांचा बनाया है जिसे सत्ता के ऐसे केंद्रीकरण को रोकने के लिए तैयार किया गया है।
हमारी व्यवस्था सत्ता के अलग और विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करती है जिनमें से प्रत्येक की अपनी जवाबदेही है। कार्यपालिका, विधायिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका चुनावों के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका, एक अलग शाखा है जो न्यायिक समीक्षा की एक कठोर, कभी-कभी धीमी प्रक्रिया और कुछ चरम स्तर के मामलों में संसदीय महाभियोग के माध्यम से अपने कार्यों के लिए जवाबदेह है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, उन्हें मनमर्जी से हटाने तक नहीं होता है। यह महत्त्वपूर्ण अंतर ही वास्तव में न्यायिक स्वतंत्रता का सार है।
हम यही संरचना अन्य संरक्षक संस्थानों’ जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के संदर्भ में भी देखते हैं। जहां तक पद से हटाने की बात है तो पहले दो संस्थान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर हैं। यूपीएससी के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय ने जांच की हो और यह बताया हो कि सदस्य को हटाया जाना चाहिए।
संविधान स्पष्ट रूप से उस संस्था का उल्लेख नहीं करता है जिसे दुनिया के अन्य हिस्सों में ‘सरकार की चौथी शाखा’ और भारत में सांविधिक नियामकीय प्राधिकरण (एसआरए) कहा जाता है। हालांकि, ऊपर बताए गए सिद्धांत एसआरए पर भी समान रूप से लागू होते हैं। एसआरए को संसद द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए बनाया जाता है जिनके लिए विशेषज्ञता, निरंतरता और राजनीतिक तटस्थता की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे बाजार विकसित हुए और उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता बढ़ी, भारत के प्रबुद्ध संसद सदस्यों द्वारा कई एजेंसियां बनाई गई। इस संरचना के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) जैसे सांविधिक नियामकीय प्राधिकरण सरकार का अंग नहीं हैं। हालांकि वे अक्सर सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं का नियमन करते हैं।
उनके परिचालन की स्वायत्तता, कोई चयन का विषय नहीं है बल्कि यह एक संरचनात्मक आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर आरबीआई की भूमिका पर विचार करते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। इसके लिए अक्सर इसे राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं भले ही इस कदम से निकट भविष्य में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी हो जाए और ये फैसले सत्तारूढ़ दल को पसंद न आएं, जैसे कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला यदि कार्यपालिका, ब्याज दर नीति पर असहमत होने पर आरबीआई गवर्नर को बर्खास्त कर सके, तब केंद्रीय बैंक अपनी विश्वसनीयता और अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक हित में कार्य करने की अपनी क्षमता गंवा देगा। बाजार भी इसे तुरंत भांप लेगा, जिससे निवेशकों का भरोसा कम होगा और आखिरकार आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी।
इसी तरह, प्रतिभूति बाजारों तक पहुंच, म्युचुअल फंडों के विनियमन, विलय और अधिग्रहण, स्पेक्ट्रम के आवंटन आदि पर निर्णय जानबूझकर, रोजमर्रा की राजनीति से दूर रखे गए हैं और इनकी जिम्मेदारी विशेषज्ञ सांविधिक नियामकीय प्राधिकरणों को सैपि गए हैं।
भारतीय कानूनी ढांचा, सभी नियामक प्रमुखों को हटाने के बारे में उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसी सिद्धांत को दर्शाता है। केवल एक एसआरए कानून यानी ‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम’ में यूपीएससी सदस्य को हटाने जैसे ही पहले उच्चतम न्यायालय की जांच की आवश्यकता बताई गई है। हालांकि, व्यवहारिक तौर पर हमारे पास अमेरिका की हाल की घटनाओं जैसी स्थिति नहीं आई है।
यह मानना कि लोकतांत्रिक जवाबदेही, इन निकायों पर कार्यपालिका के नियंत्रण की मांग करती है, एक भ्रामक तर्क है। सच्ची लोकतांत्रिक जवाबदेही, कार्यपालिका के पास पूर्ण शक्ति होने से नहीं जुड़ी है। वास्तव में इसका संबंध नियंत्रण और संतुलन के एक तंत्र के भीतर, एसआरए सहित सभी एजेंसियों को उनके प्रदर्शन के लिए जवाबदेह ठहराने से जुड़ा है। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की सिफारिशों के आधार पर ही एसआरए की जवाबदेही कई स्तंभों के हिसाब से तैयार की जानी चाहिए।
किसी भी अन्य कॉरपोरेट निकाय की तरह, सांविधिक नियामक प्राधिकरणों को सबसे पहले ऐसे बोर्ड के प्रति जवाबदेह होना चाहिए जिसका गठन सावधानीपूर्वक किया गया हो। इस मामले में भारत को अभी बहुत आगे जाना है। सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड की तरह, नियामकीय बोर्ड में भी बड़ी संख्या में सरकार से स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता है। एसआरए के सभी आदेश, एक विशेषज्ञ न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने योग्य होने चाहिए। एसआरए के विधायी कार्य, संसदीय समितियों की विस्तृत जांच के अधीन होने चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट और सीएजी द्वारा व्यापक ऑडिट के आधार पर एसआरए की पूर्ण संस्थागत जवाबदेही संसद के प्रति होनी चाहिए। स्वतंत्र शोधकर्ता और अकादमिक आलोचक इन स्तंभों में अंतिम पायदान पर खड़े हैं।
संस्थागत स्वतंत्रता का क्षरण, एक धीमी और घातक प्रक्रिया है, जिसे अक्सर शब्दाडंबर वाली दक्षता और जवाबदेही के तर्क से छिपाया जाता है। अमेरिका का मामला वास्तव में एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि जब कार्यपालिका के राजनीतिक एजेंडे और किसी नियामक के तकनीकी कार्य के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं तब क्या होता है। इसका नुकसान केवल संस्था को ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और जनता के भरोसे को भी होता है।
भारत में हमारे पास अधिकतर, संस्थागत स्वतंत्रता की एक मजबूत परंपरा रही है। हालांकि, हाल के वर्षों में नियामक निकायों पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है। हमें सत्ता के केंद्रीकरण के प्रलोभन का विरोध करना चाहिए और इसके बजाय उन संस्थागत सुरक्षा उपायों को मजबूत करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे नियामक प्राधिकरण बिना किसी डर या पक्षपात के अपना काम कर सकें।
सरकार की ‘चौथी शाखा’ की स्वतंत्रता कोई विलासिता की बात नहीं है बल्कि यह हमारे लोकतंत्र का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। और एक स्थिर और समृद्ध भारत के लिए यह एक ऐसी जरूरी अपेक्षा है जिससे समझौता नहीं किया जा सकता है।
Date: 24-09-25
कसौटी पर कानून
संपादकीय

अभिव्यक्ति का अधिकार लोकतंत्र का जीवन- तत्त्व है। अगर किसी भी वजह से इस अधिकार को बाधित किया जाता है, तो इसका अंतिम नुकसान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को होगा। हालांकि कई बार ऐसी स्थितियां सामने आती हैं, जब किसी व्यक्ति की टिप्पणी को उसकी अभिव्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, लेकिन वह किसी अन्य व्यक्ति की छवि को चोट पहुंचाती दिखती है। शायद यही वजह है कि कई बार अभिव्यक्ति की सीमा का भी सवाल उठाया जाता रहा है। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहे हैं, जिनमें किसी टिप्पणी को कोई व्यक्ति अपनी मानहानि के तौर पर देखता है और ऐसा करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। यानी यह संभव है कि एक व्यक्ति के अपने विचारों की अभिव्यक्ति को कानून के मुताबिक किसी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की श्रेणी में रखा जाए। मगर यह भी सच है कि इससे संबंधित कानून को स्वतंत्र आवाजों को दबाने और गैरजरूरी तरीके से परेशान करने के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए इस संबंध में जो कहा है, वह अभिव्यक्ति के अधिकार के संदर्भ में बेहद अहम साबित हो सकता है। एक समाचार वेबसाइट से जुड़े मामले में अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपराधिक मानहानि को अब अपराध की श्रेणी से हटाने का समय आ गया है। अदालत की यह टिप्पणी संबंधित वेबसाइट पर वर्ष 2016 में प्रकाशित एक लेख को लेकर दायर आपराधिक मानहानि के मामले में सामने आई। भारत उन देशों में है, जहां मानहानि को कानूनन अपराध माना जाता है। हालांकि कुछ अन्य देशों में यह मामला कैवल नागरिक विवाद है, जिसमें मुआवजे की मांग की जा सकती है। भारत में इससे संबंधित कानून का असर इस रूप में देखा जाता है कि अक्सर राजनीतिक स्तर पर किसी संदर्भ में दो पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते हैं तो उसमें कोई एक पक्ष आरोपों को अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि बता कर कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं, जिनमें वास्तव में जानबूझ कर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में इस आरोप में घिरे व्यक्ति के खिलाफ शिकायत का कोई मजबूत आधार नहीं पाया जाता। वहीं इस कानून के तहत दर्ज मुकदमों के जरिए स्वतंत्र स्वरों को बाधित करने के मामले आम पाए जाते हैं। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को कसौटी पर रखा है।
गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2016 में शीर्ष अदालत ने ही एक मामले में आपराधिक मानहानि से संबंधित कानून को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। अब इसी अदालत ने जिस तरह मानहानि को अपराध की श्रेणी से हटाने की बात कही है, उसके अपने आधार हैं। यह छिपा नहीं है कि इस कानून का सहारा लेकर पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विरोधियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। कई बार किसी ऐसी टिप्पणी को भी मानहानिकारक बता दिया जाता है, जो तथ्यों पर आधारित होती हैं या उससे कोई बहस खड़ी हो सकती है। इस बात की संभावना हो सकती है कि कोई व्यक्ति किसी खास बयान या समाचार को अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला माने, लेकिन अगर वह बयान या समाचार व्यापक जनहित के सवालों से जुड़ा है, तो उस पर विचार किया जाना और सही पक्ष सामने लाना देश की लोकतांत्रिक जड़ों को ही मजबूत करेगा।
Date: 24-09-25
जाति से मुक्ति का मार्ग
संपादकीय
अगर यह प्रयास गंभीर है और इसका अनुपालन भी उतनी ही गंभीरता से होने वाला है, तो इसकी दिल खोल कर प्रशंसा की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक नोटिसों से सभी जातिगत संदर्भों को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। वाहनों पर जाति आधारित स्टिकर लगवाने या नारे लिखवाने वालों पर भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है। हालांकि यह कार्रवाई स्वतः स्फूर्त होने की बजाय इलाहाबाद हाई कोर्ट के रोष से बचने के लिए की गई है। सभी जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दे दिए गए हैं। इसका उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव खत्म करना है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने निर्देश दिया है कि आरोपियों की जाति पुलिस रजिस्टरों, केस विवरण, गिरफ्तारी दस्तावेज या पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर दर्ज नहीं की जानी चाहिए। यह निर्देश हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है, और तत्काल प्रभाव से लागू है। आदेश देख कर लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश को जातियों के जंजाल से मुक्ति मिलने ही वाली है। अधिकारियों को कस्बों और गांवों में ऐसे बोर्ड या संकेत हटाने के लिए भी कहा गया है, जो जातिगत पहचान का महिमामंडन करते हैं, या क्षेत्र या जाति विशेष से संबंधित बताते हैं। राज्य में राजनीतिक उद्देश्यों वाली जाति- आधारित रैलियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि जातिगत गौरव या घृणा को बढ़ावा देने वाली सोशल मीडिया सामग्री पर कड़ी नजर रखी जाएगी। प्रवीण छेत्री बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस को आरोपी व्यक्तियों की जाति का उल्लेख नहीं करने का निर्देश दिया था और राज्य को सार्वजनिक और डिजिटल माध्यमों में जाति का महिमामंडन रोकने का निर्देश दिया। सवाल है कि क्या आदेश का अनुपालन संभव हो पाएगा? हजारों सालों से यूपी ही नहीं, पूरे देश में जातिगत भेदभाव का कीड़ा लगा हुआ है। नाम से पहले ‘जाति’ पूछने की मानसिकता का क्या होगा? आज भी कथित ऊंची जातियों के गांवों में कोई ‘छोटी जात’ वाला कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। इन लोगों का शादियों में घोड़ी चढ़ना आज भी भारी पुलिस सुरक्षा के बिना संभव नहीं है। इस आदेश के अनुपालन के लिए भारी जोर-जबरदस्ती देखने को मिलने वाली है। यह बुराई इतने गहरे पैठ चुकी है कि लोग पिट कर भी गौरवान्वित महसूस करेंगे।
Date: 24-09-25
फलस्तीन के हक में
संपादकीय
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में फलस्तीन और इजरायल के लिए दो राष्ट्र के सिद्धांत पर आयोजित शिखर सम्मेलन में कई बड़े देशों ने जिस तरह फलस्तीन को आधिकारिक मान्यता देने का एलान किया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह एक रुका हुआ फैसला है, जिसे पश्चिम के देशों ने पहली बार इस स्तर पर कुबूल किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फलस्तीन को मान्यता देते हुए सही कहा कि शांति का समय आ गया है। इसके पहले ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, स्पेन आदि कई मुल्कों ने इसे मान्यता देने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने उचित ही कहा है कि एक देश के रूप में मान्यता फलस्तीनियों का अधिकार है, कोई उपहार नहीं। उन्हें यह दर्जा न देना दरअसल हमास जैसे चरमपंथियों के लिए एक तोहफा होगा, क्योंकि फिर वे इसकी आड़ में अपने कुत्सित कृत्य जारी रखेंगे और यह पूरा क्षेत्र अस्थिर बना रहेगा। दुनिया के तमाम अमनपसंद देश और लोग लगातार कहते रहे हैं कि इजरायल और फलस्तीन के लोगों से इंसाफ का तकाजा यही है कि दुनिया दोनों देशों को मान्यता दे और ये दोनों पड़ोसी मुल्क के रूप में शांति से साथ-साथ रहें ।
हालांकि, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यह समाधान मंजूर नहीं। उन्होंने न सिर्फ फलस्तीन राष्ट्र के अस्तित्व को मानने से साफ इनकार किया है, बल्कि उसे मान्यता देने वाले देशों को प्रकारांतर से धमकाया भी है। नेतन्याहू के इसी कटु तेवर ने उन देशों को भी प्रेरित किया है, जो कुछ समय पहले फलस्तीन के पक्ष में खड़े होने को तक यहूदी समुदाय के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के मद्देनजर इजरायल से सहानुभूति रखते थे। नेतन्याहू से पूर्व के तमाम इजरायली प्रधानमंत्रियों ने हमास और हिज्बुल्ला का मुकाबला करते हुए वैश्विक समुदाय से हमेशा नैतिक समर्थन की अपेक्षा की और उन्हें मिला भी, क्योंकि दुनिया हर तरह के आतंकी संगठन का अंत चाहती है। मगर अक्तूबर 2023 की वारदात के बाद नेतन्याहू सरकार की कार्रवाइयां अपना औचित्य गंवाती गई।
अमानवीयता की हद तक उसकी आक्रामकता ने यूरोप के देशों को सख्त रुख अपनाने को बाध्य किया है। आज इजरायल के साथ गिने- चुने देश खड़े हैं, जबकि दशकों बाद पश्चिम एशिया के देशों में फलस्तीन के मुद्दे पर ऐसी एकजुटता दिखी है।
निस्संदेह, आज भी तेल अवीव को अमेरिका का समर्थन हासिल है, मगर कतर पर हवाई हमले करके नेतन्याहू ने वाशिंगटन के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। इसकी तस्दीक इस तथ्य से हो जाती है। कि संयुक्त राष्ट्र के इस एकदिवसीय सम्मेलन के आयोजक सऊदी अरब और फ्रांस थे, जिनके वाशिंगटन से काफी गहरी समझ रही है। अब अमेरिका को छोड़ सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य- रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, फलस्तीन को पूर्ण राष्ट्र बनाने के पक्ष में हैं। भारत समेत संयुक्त राष्ट्र के तीन-चौथाई देश पहले ही उसे मान्यता दे चुके हैं। ऐसे में, अमेरिका के लिए स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र के लक्ष्य को लंबे समय तक रोके रखना शायद संभव न हो। यही नहीं, इटली समेत दुनिया के तमाम तटस्थ देशों में इजरायल से कारोबारी रिश्ता सीमित करने का दबाव भी बढ़ रहा है। अब तेल अवीव को तय करना है कि वह दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहेगा या अमेरिका के भरोसे अलग-थलग होना पसंद करेगा, क्योंकि दुनिया मान चुकी है कि आज या कल दो स्वतंत्र देश ही इस समस्या का स्थायी समाधान है।
Date: 24-09-25
अब शांति की गुहार लगाते नक्सली
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
इन दिनों छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के माओवाद प्रभावित इलाकों के कुछ पर्चे और ऑडियो संदेश चर्चा में है, जिनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के शीर्ष नेतृत्व में से एक अभय की तरफ से जारी किया गया है। इनमें स्पष्ट रूप से हथियार डालने और मुख्यधारा की पार्टी बनकर देश की राजनीतिक प्रक्रिया में शरीक होने की इच्छा जाहिर की गई है।
इनमें सरकार से यह अपील भी की गई है कि उनके खिलाफ चल रहे अभियान एक महीने के लिए स्थगित कर दिए जाएं, जिनसे दुर्गम इलाकों में फैले उनके नेतृत्व को आपस में सलाह-मशविरा करने का मौका मिल जाए। कई लोगों की राय में इन अपीलों की विश्वसनीयता संदिग्ध है, मगर एक समय छत्तीसगढ़ आदिवासी महासभा के अध्यक्ष रह चुके मनीष कुंजाम के मन में इसको लेकर कोई दुविधा नहीं है। वह मानते हैं कि ये माओवादी नेतृत्व द्वारा ही जारी किए गए हैं और उनके अनुसार, कारण स्पष्ट है अब सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करने वालों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
बीते कुछ वर्षों में कई बार माओवादियों ने बुद्ध-विराम की अपील जारी की थीं और सरकार की तरफ से हर बार इसे खुद के खिलाफ चल रहे अभियानों को फौरी तौर पर स्थागित कराने और अपने को पुनर्गठित करने के प्रयास के तौर पर लिया गया। एक मौके पर तो तेलंगाना सरकार के कई महत्वपूर्ण अंगों और नागरिक अधिकार संगठनों द्वारा भी प्रयास किया गया कि युद्ध विराम करा दिया जाए, पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में चल रहा अभियान रोका नहीं गया। उनके निर्देशन में चल रहा ‘ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन अपने निर्धारित लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक माओवादियों के पूर्ण सफाये को हासिल करने के लिए जारी रहा।
खास तौर से पिछले दो वर्षों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाया है। इनमें गुजरी मई में पार्टी के महासचिव नंदाला केशव राव उर्फ बसवराजू की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु उनके लिए सबसे बड़ा आघात था। अपने शीर्ष नेता के मारे जाने के बाद काडर की शुरुआती प्रतिक्रिया जरूर गुस्से से भरी थी और उन्होंने कुछ बड़ी कार्रवाइयां करने की कोशिश भी की, पर जल्द ही उनकी प्रतिक्रिया फिर से शांति अपीलों में तब्दील हो गई। माओवादियों के ताजा युद्ध-विराम संबंधी प्रस्ताव पर अभी तक सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है, पर लगता यही है कि वह अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी और घोषित लक्ष्य को 31 मार्च के पहले ही हासिल कर लेगी।
अब जब दुस्साहसिक वामवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, हमें उन कारणों पर विचार करना होगा, जिनके चलते देश के कुछ हिस्सों में जनता को अपनी आवाज सुनाने के लिए लंबे समय तक हथियार उठाना पड़ा। यह इसलिए भी जरूरी है कि चार दशकों से अधिक चला यह संघर्ष सौ से अधिक जिलों में जारी रहा और इसमें दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। मृतकों की संख्या चीन या पाकिस्तान से हुए बुद्ध की मौतों से अधिक है।
इस हिंसा का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने से कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने वाले कोई साधारण अपराधी नहीं थे। सिर्फ उनके शीर्ष नेतृत्व का प्रोफाइल देखें, तो हम पाएंगे कि वे सभी उच्च शिक्षित और खास तरह के आदशों से अनुप्राणित व्यक्ति थे। खुद महासचिव बसवराजू 1980 के दशक में तेलंगाना में वारंगल के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के मेधावी छात्र थे और रैडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के प्रभाव में आकर इस आंदोलन से जुड़े थे। गदर या वरवर राव जैसे बहुत से महत्वपूर्ण तेलुगू कवियों और नाटककारों का समर्थन भी इन्हें हासिल था। इसलिए इस सशस्त्र उभार को सिर्फ अपराधियों की हरकतें कहना उचित नहीं होगा।
ऐसा क्या था, जिसने इतने मेधावी छात्रों को इस आग में धकेल दिया? एक कटु सत्य है कि हमारे देश के वे आदिवासी इलाके, जहां माओवादी सक्रिय हैं, आजादी के बाद वही विकास की धारा से पूरी तरह अछूते रहे। जीवित रहने के लिए जंगलों पर निर्भर इन लोगों का जीवन प्रतिकूल वन कानूनों ने और मुश्किल बना रखा था। जब उन्होंने हथियार उठाए, तभी सरकारों को पता चला कि वे भी मनुष्य हैं और उन्हें भी सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा या रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओ की जरूरत है। पिछले कुछ दशकों में पुलिस कार्रवाइयों के अतिरिक्त आदिवासी गांवों तक ये सुविधाएं पहुंची हैं और उनका सकारात्मक असर भी पड़ा है। सड़कों और मोबाइल टावरों से संभव हुए सुगम संचार ने गांव वालों की जिंदगी तो सरल बनाई डी, सुरक्षा बलों को भी बेहतर ढंग से कार्रवाई करने का अवसर प्रदान कर दिया है। शायद इसीलिए माओवादी अतिम दम तक इन सुविधाओं का विरोध करते रहे।
सशस्त्र आंदोलन की विफलता से यह भी स्पष्ट हो गया है कि अब किसी भी समूह या संगठन के लिए संभव नहीं रह गया है कि वह हथियारों के बल पर राज्य सत्ता पर कब्जा कर ले। माओवादी नेताओ ने युद्ध विराम की अपनी हर अपील के साथ यह भी कहा है कि वे हथियार छोड़कर जनता के बीच जाना चाहते हैं, अर्थात अन्य राजनीतिक दलों की तरह ये भी चुनावों मे भाग लेने के लिए तैयार हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि शीघ्र ही हमें मुख्यधारा की एक और कम्युनिस्ट पार्टी मिलेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि उसके जिन काडरों ने पिछले दिनों पुलिस के सामने समर्पण किया है, उनमें से कितने चुनावी राजनीति में उसके साथ आएंगे, पर इतना जरूर है कि अलग-अलग राज्यों के जिन क्षेत्रों में माओवादियों ने अपना प्रभाव बना रखा है, उनमें चुनावों में उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति दिख सकती है।
कुल मिलाकर, गृह मंत्री अमित शाह का दावा सही होने जा रहा है और 31 मार्च, 2026 तक माओवादियों का पूरी तरह से सफाया हो सकता है। अभी तक सरकार ने शांति के प्रस्तावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और उसके सक्षम सूत्र सिर्फ यही कह रहे हैं कि माओवादियों को बिना शर्त हथियार डालकर समर्पण करने वालों को मिलने वाली सरकारी सहायता का लाभ उठाना चाहिए। यह एक ऐसी जिद है, जिसे छोड़कर लड़ाकों से बातों कर हथियार डलवाना सबके हित में है। इससे बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को माओवाद प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सरकार दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकती है, जनता को हिंसा से मुक्ति मिलेगी और माओवादी नेतृत्व को भी हथियार डालने का एक सम्मानजनक रास्ता मिल जाएगा। शांति से देश के 200 से अधिक जिलों में विकास की एक नई गाथा शुरू होगी।
