
31-05-2019 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Bring Transparency To Statistics System
ET Editorials
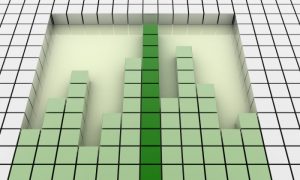
The government’s think tank Niti Aayog is in touch with the World Bank to modernise India’s statistical system and align it with global best practices, says its vice-chairman Rajiv Kumar. A revamp is certainly warranted, so that up-to-date, even real-time, data can be garnered for informed policy-making. More importantly, we need systems for timely and reliable government statistics that are seen as objective, and free from any bias, deemed or real.
The reported plan is to merge the National Sample Survey Office (NSSO) with the Central Statistics Office (CSO), two organisations in the ministry of statistics and programme implementation, to form the National Statistics Office (NSO). The idea it seems is to streamline operations for statistical survey and data compilation, which appears sensible. The NSO must, of course, boost transparency in the entire exercise of estimating national statistical data, including gross domestic product (GDP) figures and employment trends. The CSO has come out with a new GDP series with 2011-12 as the new base year since 2015. But it is only last year that the GDP back series for previous years was put out, and there has been avoidable controversy about GDP estimation methodology, which has resulted in reduced GDP growth prior to 2014, and heightened growth since.
It is possible that the new GDP price deflators, which are sector-specific, lead to more accurate estimates. Similarly, change in frequency and scope of employment surveys may be quite appropriate. But such statistical innovation cannot remain opaque. They need to be widely debated and critiqued by the profession of statisticians, so that there is consensus on the way forward and comparability. The NSO surely needs to setup an expert body for the very purpose.
![]() Date:31-05-19
Date:31-05-19
ढांचागत निवेश में जादुई ताकत लाने की क्षमता
ढांचागत परियोजनाओं में निवेश के लिए निजी पूंजी को दोबारा प्रोत्साहित करना मौजूदा वक्त की जरूरत है।
विनायक चटर्जी , (लेखक ढांचागत सलाहकार फर्म फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं)
किसी भी नई सरकार की ढांचागत क्षेत्र के लिए क्या नीति होनी चाहिए? फासला कहां पर है? और इस फासले को दूर करने के लिए किन सुधारों की जरूरत है? आज के समय में ये सवाल काफी अहम हैं। ढांचागत क्षेत्र में निवेश वर्ष 2007 और 2012 के बीच सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब सात फीसदी बढ़ा जबकि उससे पहले के पांच वर्षों में पांच फीसदी वृद्धि हुई थी। ढांचागत निवेश में आई इस उछाल की प्रमुख वजह निजी क्षेत्र की भूमिका थी। पांच साल पहले की अवधि के मुकाबले ढांचागत निवेश में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 15 फीसदी तक बढ़ गई।
लेकिन अगर पीछे की तरफ नजर डालें तो एक गंभीर मसले के चलते वह वृद्धि टिकाऊ नहीं थी। वह ढांचागत ‘बूम’ बड़ी नीतिगत एवं संरचनात्मक खामियों के बावजूद आया था। इस वजह से ऐसी वृद्धि का धीरे-धीरे लुप्त होना अपरिहार्य था। भूमि अधिग्रहण में मुश्किल होने, जोखिम आवंटन बढऩे, विभिन्न एजेंसियों से अनगिनत अनापत्तियां लेने और ढांचागत परियोजनाओं में वाणिज्यिक बैंकों की प्रभावी भूमिका होने से लेकर ईंधन एवं वितरण संबंधी अड़चनें तक ऐसी कमजोरियां रहीं जिनसे पार पाना मुश्किल था।
इस तरह वर्ष 2013 के बाद जीडीपी प्रतिशत के तौर पर ढांचागत निवेश की हिस्सेदारी खिसकते हुए केवल पांच फीसदी ही रह गई। ढांचागत निवेश में निजी क्षेत्र का अंशदान वर्ष 2013-18 के बीच 48 फीसदी रहने का आकलन किया गया था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र ने इस कमी की भरपाई की है। आगे चलें तो मौजूदा राजकोषीय स्थिति देखते हुए इसकी काफी कम गुंजाइश नजर आती है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अगले पांच वर्षों में ढांचागत क्षेत्र में काफी खर्च करने की बात कही है। भाजपा ने वर्ष 2024 तक एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया है। अगर आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने वाले ऐसे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करना है तो निजी क्षेत्र को फिर से बड़ी भूमिका निभानी होगी। और इसका मतलब है कि पहले निजी क्षेत्र को पीछे हटने के लिए मजबूर करने वाली संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करना होगा।
संयोग से किसी भी नई सरकार को फिर से कमजोरियों की पहचान या नए समाधान तलाशने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने ढांचागत क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी में नई जान फूंकने के लिए अध्ययन का काम विजय केलकर को सौंपा था। वर्ष 2015 में जारी उस रिपोर्ट में की गई कई सिफारिशें आज भी प्रासंगिक हैं। केलकर समिति ने परियोजना समीक्षा समिति (पीपीपी) बनाने के साथ ही ढांचागत पीपीपी निर्णयन अधिकरण (आईपीएटी) के गठन की भी सिफारिश की थी। ये दोनों निकाय मिलकर आर्थिक संदर्भ या हालत बदलने की स्थिति में किसी परियोजना की शर्तों में बदलाव की जरूरत पर गौर करेंगे। ऐसा होने पर कई परियोजनाओं को पेश आ रही अहम समस्या दूर की जा सकेगी। स्पष्ट संस्थागत प्रक्रियाओं का अभाव होने से अनुबंधों पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है। ढांचागत क्षेत्र में यह समस्या खास रही है जहां रियायती समझौते 30 साल और उससे आगे भी जा सकते हैं और समझौते पर हस्ताक्षर के संदर्भ पहचान से परे तक बदल चुके हैं।
समिति ने यह साफ किया था कि ढांचागत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र नियामक होना निहायत ही जरूरी है। रेलवे जैसे क्षेत्रों में यह एक खास गंभीर मुद्दा है। प्रïभावी सार्वजनिक इकाई भारतीय रेलवे रेल परिवहन का नियामक, डेवलपर एवं नीति-निर्माता तीनों ही है जिससे हितों के टकराव की गंभीर स्थिति बन जाती है। यह सड़कों के लिए भी उतना ही सही है। और नियामक की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में भी ‘स्वतंत्र’ का तमगा अक्सर संदेह के घेरे में होता है। समिति ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में कुछ संशोधन करने का भी प्रस्ताव रखा था ताकि फैसलों से जुड़ी असली वाणिज्यिक गलतियों के लिए अधिकारियों को दंडित न होना पड़े।
केलकर समिति ने अपनी सिफारिशों को महज विवाद निपटान और नियामकीय मुद्दों तक ही सीमित नहीं रखा था। उसने पीपीपी के मुख्य ढांचे पर भी गौर किया था। इस बारे में समिति की प्रमुख सलाह इस समझ की थी कि निजी क्षेत्र कुछ खास तरह के जोखिम तो खुद उठा सकते हैं लेकिन कुछ जोखिम वे नहीं ले सकते हैं। रियायती करारों में ‘एक ही ढांचा सबके लिए मुफीद होता है’ वाला मॉडल परियोजना-केंद्रित एवं क्षेत्र-केंद्रित संदर्भों का ध्यान नहीं रखता है। मसलन, एक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य ऐसा नहीं है जिसे कोई निजी कंपनी अपनी सामान्य कारोबारी गतिविधियों में अंजाम देती है लिहाजा संबंधित सरकार को ही यह जोखिम उठाना चाहिए। निविदा के दस्तावेजों में यह साफ तौर पर वर्णित होना चाहिए कि किस तरह के हालात में पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से पुनर्विचार होगा?
केलकर समिति की रिपोर्ट में ढांचागत परिदृश्य के एक और प्रमुख बिंदु को जगह दी गई थी। इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) ढांचे पर बनी कई परियोजनाएं असल में निर्माण के दौर से आगे बढ़ते हुए परिचालन एवं रखरखाव (ओऐंडएम) के दौर में आ चुकी हैं। ऐसे में उनकी तरफ से उपभोक्ताओं को दी जानी सेवाओं का सटीक एवं पारदर्शी होना निहायत ही जरूरी है। ऐसे ओऐंडएम अनुबंधों का प्रबंधन ऐसी गतिविधियों में अनुभव एवं दक्षता रखने वाली निजी कंपनियों के हवाले कर दिया जाना चाहिए। यह बात परिसंपत्ति-पुनर्चक्रीकरण नीति के तहत सरकारी स्वामित्व वाली इकाइयों में सरकार के पैसे लगाने की स्थिति में भी सही है।
समिति की रिपोर्ट आने के चार साल बाद यह साफ हो चुका है कि केलकर रिपोर्ट एक व्यावहारिक एवं बुनियाद खड़ा करने वाला दस्तावेज है। आज भी यह रिपोर्ट अगले कुछ वर्षों के लिए ढांचागत क्षेत्र में निवेश के भविष्य को लेकर एक साफ रोडमैप तैयार करती है। कुछ अन्य बिंदुओं को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। मसलन, बिना सोचे-समझे बोली लगाने से रोकना या एक मान्यता-प्राप्त ढांचे के रूप में स्विस चैलेंज की अनुमति देना या फिर ‘प्लग ऐंड प्ले’ जैसे अधिक अनुकूल माने जाने वाले पीपीपी ढांचे को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। मौजूदा समय में नई सरकार के लिए पीपीपी-पुनर्जीवन प्रक्रिया लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने की जरूरत है।
जाति का दंश
संपादकीय

मुंबई के एक अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर पायल तडवी की आत्महत्या ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर किया है कि आजादी के सात दशक बाद भी हमारे समाज में वंचित तबके के प्रति बराबरी और इंसाफ की भावना का पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो सका है। मुंबई के बीवाइएल नायर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर पायल तडवी ने अपनी तीन वरिष्ठ डॉक्टरों की प्रताड़ना से तंग आकर बाईस मई को आत्महत्या कर ली थी। उत्पीड़न की शक्ल केवल पद या कद के संवेदनहीन बर्ताव से नहीं जुड़ी थी, बल्कि खबरों के मुताबिक रैगिंग के नाम पर पायल को अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए उन पर जातिसूचक फब्तियां कसी जाती थीं। पायल तडवी आदिवासी समुदाय की भील जाति की पृष्ठभूमि से थीं और उनके परिवार ने काफी संघर्ष से उन्हें डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए भेजा था। लेकिन चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्र में अपनी काबिलियत के बूते जगह बनाने के बावजूद उन्हें जाति के आधार पर होने वाले उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जाहिर है, यह सामाजिक और जातिगत भेदभाव से जुड़ा मामला है, जिसने पायल को खुदकुशी कर लेने पर मजबूर कर दिया।
विडंबना यह है कि इसकी शिकायत अस्पताल के संबंधित जिम्मेदार लोगों से की गई थी, लेकिन वक्त पर कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा गया। अब अस्पताल प्रबंधन या कोई भी अगर घटना पर अफसोस जाहिर करता है या कार्रवाई का भरोसा देता है तो इसकी क्या अहमियत है! मामले के तूल पकड़ने के बाद अब जाकर उन तीनों आरोपी महिला डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत मुकदमा चलेगा। लेकिन शिकायत को समय पर गंभीरता से नहीं लेने की वजह से क्या अस्पताल प्रबंधन को भी कठघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? आखिर किन वजहों से अस्पताल का प्रबंधन अपने परिसर में नौकरी या पढ़ाई के लिए कमजोर तबकों से आने वाले लोगों के बीच बराबरी और भेदभाव से मुक्त माहौल मुहैया करा पाने में नाकाम साबित हुआ? यह समझना मुश्किल है कि विज्ञान पर आधारित एक विषय में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही तीनों आरोपी महिला डॉक्टरों के भीतर अपने उच्च कही जाने वाली जाति से होने का दंभ कैसे बरकरार था और उनके लिए अपनी ही एक सहयोगी को जाति के आधार पर इस हद तक प्रताड़ित करना कैसे संभव हुआ कि उसकी सहनशक्ति जवाब दे गई?
सही है कि कुछ घटनाओं के आधार पर सब तरफ एक-सी स्थिति होने को अंतिम सच नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि विकास के तमाम दावों के बीच जातिगत भेदभाव के ऐसे बर्ताव न केवल देश के पिछड़े माने जाने वाले इलाकों में रहने वाले समुदायों, बल्कि आधुनिकता और उच्च शिक्षा की चकाचौंध में भी अक्सर सामने आते रहते हैं। यह तब है जब दलित-वंचित तबकों और आदिवासियों के संरक्षण के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था है, कानूनी प्रावधान हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ऐसे कानूनी संरक्षण नहीं होते तब खुद को उच्च कही जाने वाली जाति से मानने वालों का व्यवहार दलित-वंचित जातियों-तबकों के लोगों के प्रति क्या होता! सवाल है कि इस तरह के जातिगत विद्वेष और दुराग्रहों पर आधारित मानसिकता के साथ जीते हुए क्या हम एक सभ्य और संवेदनशील समाज होने का दावा कर सकते हैं? मुंबई की घटना में अगर समय रहते जरूरी कदम उठाए गए होते तो समाज में विकास और बराबरी के पायदान पर काफी पीछे रह गए समुदाय से आने वाली पायल आज शायद जीवित होतीं और अपनी काबिलियत से समाज और देश की सेवा कर पातीं। लेकिन जातिगत भेदभाव से संचालित नफरत की मानसिकता ने असमय ही उनकी जिंदगी छीन ली।
क्षेत्रीय गढ़ों की दरकती जमीन
राजेंद्र धोड़पकर, वरिष्ठ पत्रकार
इस आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत का विश्लेषण तमाम तरह से जारी है। इसका एक बहुत बड़ा कारक यह है कि राजनीति के जातीय समीकरणों में भाजपा ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसका दूरगामी असर भारतीय राजनीति में होगा। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद इसे देश का दूसरा बड़ा सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन कहा जा सकता है।
मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई। ये क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादातर जनता पार्टी प्रयोग की टूट-फूट से बनी थीं या कांग्रेस के केंद्रीय आधिपत्य के विरोध में स्थानीय अस्मिता के सवाल पर खड़ी हुई थीं। इन पार्टियों का आधार मुख्य रूप से पिछड़ी जातियां थीं या बसपा की तरह दलित समूह थे। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय भी भारत में अमूमन किसी पिछड़े समुदाय जैसा ही है, इसलिए मुलायम सिंह यादव या लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं के साथ मुसलमान भी जुडे़ थे। ऐसा लगने लगा था कि अब भारत की राजनीति का भविष्य इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों से जुड़ा है और कांग्रेस या भाजपा जैसी पार्टियों को अगर केंद्र में राज करना है, तो इन पार्टियों के साथ सत्ता में साझीदारी करनी पड़ेगी, और ज्यादातर राज्यों में उन्हें इन पार्टियों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। लोकसभा में भाजपा ने पिछले चुनाव में भी पूर्ण बहुमत पाया था और अब ज्यादा बड़ा बहुमत पाया है। क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा को रोकने या उसे अपने ऊपर निर्भर बनाने में नाकाम रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह इन पार्टियों के चरित्र में बदलाव है।
कभी ये क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा व्यापक समूहों का प्रतिनिधित्व करती थीं। जैसे मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में तमाम पिछड़े समूह इकट्ठे थे। यादवों के अलावा राजभर, कुर्मी वगैरह जातियां भी उनके साथ थीं। यही स्थिति राजद की भी थी, जिसके साथ पिछड़ों के अलावा कुछ दलित जातियां भी थीं। इसी तरह, उत्तर प्रदेश में बसपा व्यापक रूप से दलितों की पार्टी थी, बल्कि देश भर के दलित उसकी ओर उम्मीद से देखते थे।
अब इन पार्टियों का आधार संकुचित होता दिख रहा है। अन्य पिछड़े या दलित समुदायों को यह शिकायत होने लगी कि इन पार्टियों में किसी एक जाति को विशेष तरजीह दी जा रही है और उनकी उपेक्षा हो रही है, या सत्ता के लाभ का बराबर बंटवारा नहीं हो रहा है। इन पार्टियों का नेतृत्व किसी एक बड़े नेता या परिवार के पास ही था, इसलिए उन पर यह आरोप लगने लगा कि वे अपनी जाति को ज्यादा महत्व देते हैं। धीरे-धीरे सपा और राजद की पहचान यादवों की पार्टी तक सिमट गई। बसपा भी उत्तर प्रदेश के जाटवों की पार्टी बन गई। कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी वोक्कलिगा की पार्टी हो गई। यह समस्या हर जगह दिखी। हरियाणा में चौटाला और हुड्डा परिवारों से यह शिकायत रही कि उनकी राजनीति जाटों तक सीमित है, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस, राकांपा की राजनीति में मराठा वर्चस्व के खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा। अपना जनाधार सीमित करके ये पार्टियां अपनी ताकत भी खोने लगीं। ताकत कम होने के अंदेशे से असुरक्षित होकर नेता अपनी बुनियाद यानी अपनी जाति से और ज्यादा जुड़ते गए, जबकि अन्य जातियां उनसे और ज्यादा छिटकने लगीं। समावेशी नीति बनाने और संसाधनों के वितरण का दायरा न्यायपूर्ण ढंग से बढ़ाने की बजाय ये पार्टियां अपने खास या अपेक्षाकृत ताकतवर लोगों को खुश करके राजनीति चलाती रहीं। सामाजिक न्याय की एक सुविधाजनक व्याख्या उन्होंने अपने लोगों को रेवड़ी बांटने की कर ली। प्रभाव का दायरा बढ़ाने की बजाय अपने लोगों के प्रति वफादारी उन्हें महत्वपूर्ण लगी, जिसका नतीजा अब दिख रहा है।
ये पार्टियां अपेक्षाकृत शक्तिशाली जातियों के वर्चस्व वाली पार्टियां हैं, इसलिए सामाजिक-आर्थिक तौर पर बेहतरी की गुंजाइश भी इन जातियों के कुछ हिस्सों के लिए ज्यादा है। अक्सर जब लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर बेहतर स्थिति में पहुंचते हैं, तब उन्हें जाति के संरक्षण की जरूरत उतनी नहीं रहती या उनकी वर्गगत पहचान जातिगत पहचान के मुकाबले कुछ अधिक मजबूत हो जाती है। ऐसे में, जरूरी नहीं कि वे अपनी जाति के आधार पर ही वोट करें। हो सकता है कि वे किसी और वजह से भाजपा या अन्य पार्टी को वोट दें। ऐसा पिछले चुनाव में देखने में आया है। समृद्धि और सत्ता के असमान वितरण से वर्चस्वशाली जाति के वंचित सदस्य भी असंतुष्ट हो सकते हैं, जैसा कि जाट और मराठों के आंदोलनों में देखने में आया है। ऐसे में, वे जाति के परंपरागत नेतृत्व से छिटक भी सकते हैं। इसके अलावा, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार और एच डी देवेगौड़ा के प्रति लोगों की जो वफादारी है, वह तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, पार्थ पवार या निखिल देवेगौड़ा को विरासत में पूरी नहीं मिल सकती।
भाजपा ने बहुत मेहनत से इन क्षेत्रीय पार्टियों से असंतुष्ट पिछड़ी और दलित जातियों के बीच काम किया और उनके असंतोष को ज्यादा हवा दी। इन छोटे-छोटे समूहों का कुल संख्या बल वर्चस्वशाली जातियों के वोटों से ज्यादा बैठता है। विकास में साझीदारी और हिंदुत्व के गोंद ने इन जातियों को भाजपा के उच्चवर्णीय आधार से जोड़ दिया। इसीलिए भाजपा ने जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, उनमें वर्चस्वशाली पिछड़ी जातियां गायब हैं। उनमें कहीं ब्राह्मण, कहीं राजपूत, तो कहीं पंजाबी खत्री हैं, जो सब उच्चवर्णीय हैं।
ऐसा नहीं है कि राजनीति में पिछड़ों और दलितों का महत्व घट गया है, लेकिन उनके राजनीतिक आधार के बंट जाने से उनकी ताकत कम हुई है और नेतृत्व भी उनसे छिन जाने का खतरा खड़ा हो गया है। भाजपा के हिंदुत्व की वजह से अल्पसंख्यक भाजपा विरोधी पार्टियों को वोट देने के लिए मजबूर हैं, पर विकल्प की इच्छा उनके मन में भी है। अपने आधार को विस्तृत करने के लिए इन पार्टियों के नेताओं को अपना संकुचित नजरिया बदलना होगा, सचमुच सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अपनाना होगा और अपनी जाति के दायरे के बाहर देखना होगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई अपने सुरक्षित और आरामदेह किलों में रहकर नहीं लड़ी जा सकती।
