
29-08-2022 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:29-08-22
Date:29-08-22
Fallty Towers
Lesson from the Supertech demolition: reduce the risk borne by homebuyers, improve Rera
TOI Editorials

About 77% of total assets of an average Indian household are held in real estate. It’s the largest single investment most families make. This also makes them vulnerable to a peculiar feature of real estate – a disproportionate share of the risk is on homebuyers. Consider this version of the subvention model, a tripartite agreement betweena builder, bank and buyer. The buyer pays a part of the project cost upfront, the bank covers the residual cost and the builder underwrites EMIs till possession is handed. There are a number of cases where builders default and banks chase the hapless buyer despite the agreement detailing the obligations of all sides. In one such case, the Delhi high court this year ordered interim protection to buyers against coercive action by banks. But there are many cases.
So, any meaningful reform has to address the spread of risks among stakeholders. Of all attempts to reform, the Real Estate (Regulation and Development) Act represents the most promising one. It embodies the work of two governments and detailed discussions of parliamentary committees. The key advantages of Rera are that it brings about standardisation of contracts, reduces the information asymmetry between buyers and other stakeholders by making relevant information public and minimises misuse of upfront payments by buyers.
Rera was enacted in 2016 and can’t address older problems like that of the Supertech towers. Neither can it resolve the corruption at the level of urban bodies, which blight the dreams of many buyers. It also suffers from the general weakness in state capacity as each state needs to establish a regulatory body. Notwithstanding the challenges, Rera represents the best available solution today. It requires state governments to invest in enhancing capacity. Buyers will benefit from a fairer system, not a spectacle.
Sops for votes
Promising gifts in run-up to polls, not welfare, is the real ‘freebie’ issue
Editorial
After considering the formation of an expert body to examine the issues relating to political parties promising free goods to voters in their election manifestoes, the Supreme Court has stayed its hand and referred the issue to a three-judge Bench. Also referred for deeper consideration is the correctness of an earlier judgment in S. Subramaniam Balaji vs Tamil Nadu (2013), which ruled that making promises in a manifesto would not amount to a corrupt practice. The proceedings before a Bench, headed by the now retired Chief Justice of India N.V. Ramana, last week, offered crucial perspectives on the political economy of welfarism, socialism and pre-election promises of ‘freebies’. Over the few hearings, the Bench moved from vague references to ‘freebies’ to making rational distinctions between welfare schemes and socio-economic concessions on the one hand, and poll-time announcements of material goods and items as incentives to vote. This clarity itself was lacking in the initial stages, as omnibus references to ‘freebies’ and raillery against political parties for their approach to welfare dominated the discourse. Those who have approached the Court against irrational promises found support from the Union government. Following Prime Minister Narendra Modi making public comments disapproving of the ‘freebie’ culture, the Government’s stand is no surprise.
However, the Government was reluctant to examine the issue through discussions among political parties and favoured a judicially appointed panel. But, such a panel may not achieve much. Most parties oppose any fetters on their right to appeal to voters through means of their choice and, if elected, use their mandate to distribute finances and resources as they deem fit, subject to law and legislative approval. Therefore, it is no surprise that the Bench has included in its reference, questions on the scope of judicial intervention in the matter and whether any enforceable order can be passed. The two-judge Bench judgment in 2013 had examined the issue in the backdrop of the DMK coming to power in 2006 on a promise to distribute television sets to the poor and implementing it. It ruled that the Directive Principles of State Policy allow such schemes and that spending of public funds on them could not be questioned if it was based on appropriations passed by the legislature. It also concluded that poll promises by a party could not be termed a ‘corrupt practice’. That Bench had also rejected the argument that giving benefits to everyone, that is, the poor and the well-off, would violate the equality norm in Article 14. When it came to state largesse, it said, the rule against treating unequals as equals would not be applicable. Does this amount to implying that the Directive Principles can override fundamental rights, as the petitioners have argued? This too awaits examination.
भ्रष्टाचार की इमारतें
संपादकीय
यह सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का ही नतीजा कहा जाएगा कि नोएडा के सैक्टर 92 में एक दशक से भी ज्यादा समय से खड़ी दो बहुमंजिला अवैध इमारतों को रविवार को आखिरकार ढहा दिया गया। दोनों इमारतें सुपरटेक बिल्डर की परियोजना का हिस्सा थीं। इनके निर्माण में नियम-कानूनों की जिस तरह से धज्जियां उड़ती रहीं, वह हमारी सरकारों और शहरी विकास के निकायों यानी प्राधिकरणों की भ्रष्ट संस्कृति को उजागर करने के लिए काफी है। सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल 31 अगस्त को एक आदेश जारी कर इन इमारतों को तीन महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया था। लेकिन नोएडा प्राधिकरण को इस काम में भी एक साल लग गया! खैर, भले इस काम में देरी हुई और इस परिसर के निवासियों को सुपरटेक के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, पर इसका नतीजा न केवल सुखद रहा, बल्कि कड़ा संदेश देने वाला भी रहा। सर्वोच्च अदालत की यह कठोर कार्रवाई उन सभी भवन निर्माताओं के लिए सबक है जो पैसे के बल पर कानून के शासन को चुनौती देते रहे हैं। इन अवैध इमारतों को गिरवा कर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट सक्रियता नहीं दिखाते तो सुपरटेक का शायद कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अवैध रूप से बनी इन इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। लेकिन तब सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसे उम्मीद रही होगी कि पैसे और रसूख के बल पर यहां कुछ राहत मिल जाएगी। अगर ये इमारतें नियमों का पालन करते हुए बनाई गर्इं होतीं तो लोग अदालत जाने को क्यों मजबूर होते? न ही सुपरटेक कंपनी हारती! यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि अगर प्राधिकरण के अधिकारी मेहरबान हो जाएं तो किस तरह से बिल्डर नियम-कानून को ताक पर रखते हुए भ्रष्टाचार की इमारतें खड़ी करते चले जाते हैं। वैसे यह सुपरटेक का अकेला मामला नहीं है, ऐसे न जाने कितने ही मामले होंगे। हर शहर में विकास प्राधिकरण होते हैं जिनका काम ही शहरी नियोजन और भवन निर्माण संबंधी कामकाज देखना होता है। पर शायद ही कोई ऐसा शहर हो जो अवैध निर्माण के रोग से ग्रस्त न हो। मगर ऐसी कार्रवाई हर जगह इसलिए नहीं हो पाती कि कोई आवाज नहीं उठाता और अवैध निर्माण पर नजर रखना और उसे न होने देना जिनकी जिम्मेदारी होती है, वे खुद ही इसमें लिप्त रहते हैं। सुपरटेक परिसर के निवासी अदालत गए और लंबी लड़ाई लड़ी, इसलिए यह मामला तार्किक परिणति तक पहुंच पाया।
सुपरटेक के दोनों अवैध निर्माण तो ढहा दिए गए, पर अब सवाल यह है कि प्राधिकरण के जिन अधिकारियों की वजह से भवन निर्माण कंपनियां फलती-फूलती रहीं और अवैध निर्माण होते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार कहां तक पहुंची? सर्वोच्च अदालत ने प्राधिकरण के उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे जिनकी वजह से यह गोरखधंधा चलता रहा। हालांकि सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम बनाने की औपचारिकता पूरी कर दी थी, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई होती नहीं दिखी जो मिसाल कायम करती। जबकि इस मामले में आरोपी चौबीस अधिकारियों में से उन्नीस सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का अब तक जो शिथिल रवैया देखने को मिलता रहा है, उससे तो लगता नहीं कि किसी को सजा मिल भी पाएगी। हालांकि अगर सरकारें ठान लें तो भ्रष्टाचार की इमारतों को ढहाना असंभव नहीं!
Date:29-08-22
विलंबित न्याय
संपादकीय
एक बार फिर अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठा है। अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने अपने विदाई भाषण में अदालतों में लंबित मुकदमों को बड़ी चुनौती बताया। इससे पहले अनेक मौकों पर यह बात दोहराई जा चुकी है। पिछले कुछ सालों में प्राय: हर प्रधान न्यायाधीश ने इस मसले पर चिंता जाहिर की है। इसके अलावा आम आदमी को शीघ्र और किफायती न्याया दिलाने का संकल्प भी अनेक बार दोहराया जा चुका है। सरकार भी इस तथ्य से अनजान नहीं। कुछ मौकों पर प्रधानमंत्री भी इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। अदालतों पर मुकदमों के बढ़ते बोझ की वजहें भी सब जानते हैं। मगर हर बार ये बातें केवल आदर्श वाक्य की तरह दोहरा दी गई साबित होती हैं। इस दिशा में कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया जाता। आबादी के अनुपात में अदालतों और न्यायाधीशों का न होना पहली समस्या है। इससे पार पाने के लिए दो पाली में अदालतें लगाने, अवकाशप्राप्त न्यायाधीशों की मदद लेने, त्वरित अदालतों का गठन, लोक अदालतों की व्यवस्था आदि की गई। मगर फिर भी अपेक्षित नतीजे नहीं आ रहे। इसी के मद्देनजर न्यायमूर्ति रमण ने इस समस्या से पार पाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल की जरूरत रेखांकित की है।
हालांकि प्रधान न्यायाधीश रहते न्यायमूर्ति रमण ने अदालतों का कामकाज सुचारु बनाने के लिए काफी प्रयास किया। खाली पदों को भरने के लिए एक तरह से सरकार से टकराव भी मोल लिया। मगर नई अदालतें गठित करने और जनसंख्या के अनुपात में जजों की नियुक्ति का मामला लंबे समय से लटका पड़ा है। जजों के खाली पदों पर भर्ती को लेकर सरकारें प्राय: उदासीन बनी रहती हैं। पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से वरीयता क्रम में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए जो सूची भेजी गई थी, उसे केंद्र सरकार ने लंबे समय तक लटकाए रखा और बहुत दबाव बनाने के बाद भी पूरी सूची पर भर्ती की संस्तुति नहीं दी। उसमें वरीयता क्रम बदल दिया गया। इस तरह अदालतों में लंबित मामलों के पीछे एक बड़ा कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी भी है। फिर एक समस्या सरकारों की तरफ से दर्ज कराए जाने वाले बड़ी संख्या में वे मुकदमे भी हैं, जिनमें जमानत का प्रावधान नहीं है और जिनकी जांच आदि में कई बार जानबूझ कर देर की जाती है या सरकारों की तरफ से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता। इसी से खीझ कर खुद एनवी रमण ने एक बयान में कहा था कि सबसे बड़ी मुकदमेबाज खुद सरकार है।
इसके अलावा, बहुत सारे मामले इसलिए लंबे समय तक खिंचते जाते हैं कि उनमें कोई पक्ष इतना कमजोर होता है कि अपनी पैरवी ठीक से नहीं कर या करा पाता। जिस आम आदमी को शीघ्र और किफायती न्याय की बात एनवी रमण ने की, वह वही है। हालांकि लाखों मामले ऐसे होंगे, जिनके फैसले दो-तीन सुनवाइयों में ही तय हो जाते, मगर किसी एक पक्ष के नाहक लंबा खींचने की वजह से वे लटके रहते हैं। जमीन-जायदाद, घरेलू विवाद, छोटी-मोटी चोरी, किसी आंदोलन आदि में हिस्सेदारी वगैरह के चलते जिन लोगों पर मुकदमे किए जाते हैं, उन्हें पहली ही बार में न्यायाधीश समझ जाते हैं कि इसमें क्या फैसला दिया जा सकता है। मगर वे भी सालों खिंचते जाते हैं। जिन मामलों में कोई गंभीर सजा नहीं हो सकती, उनमें भी लोगों को वर्षों विचाराधीन कैदी के रूप में सलाखों के पीछे रखा जाता है। इस पर कब गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा, देखने की बात है।
Date:29-08-22
मशीनी दिमाग के बड़े खतरे
निरंकार सिंह
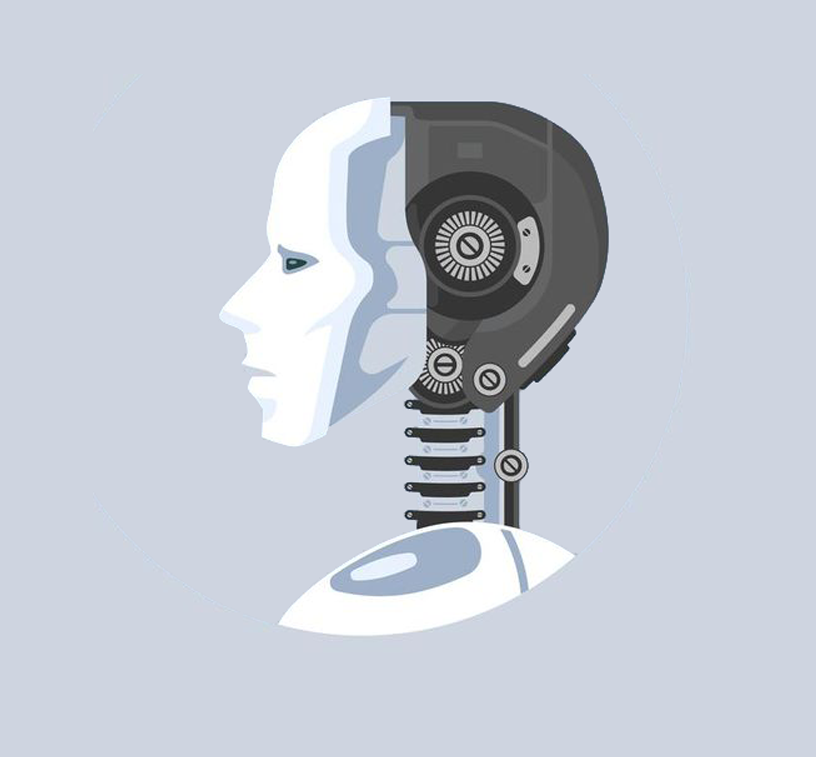
नौकरी के लिए तो करोड़ों लोग परेशान है। दुखद तो यह कि नौकरी नहीं मिलने से खुदकुशी करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में यह देखने में आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक अस्सी करोड़ नौकरियां कम हो जाएंगी। डेलोइट की एक रिपोर्ट में पता चला है की 2025 तक दस लाख से ज्यादा वकीलों की नौकरी खत्म होने वाली है। कुछ नौकरियां भी ऐसी हैं जिनके कामों को मशीनी दिमाग यानी कृत्रिम बुद्धि (एआइ) से आसानी से कराया जा सकेगाा। 2015 में गूगल ने बिना ड्राइवर के चलने वाली कार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। भविष्य में स्वचालित कारों में और सुधार होगा और ड्राइवरों की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार अमेजन ने ड्रोन के जरिए सामान भेजना शुरू कर दिया। यानी अब सामान पहुंचाने वालों की कोई जरूरत नहीं है। यह सब अभी अमेरिका में चल रहा है और लोगों को भी कोई परेशानी नहीं आती। इसी प्रकार बड़े-बड़े होटलों में भी रोबोट ही खाना परोसेंगे और खाना भी बनाएंगे। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कृत्रिम मेधा तकनीक के बढ़ते चलन से दुनियाभर में सैंतालीस फीसदी नौकरियां खतरे में हैं। मैकिनजी ग्लोबल इंस्टीट्रयूट आफ रिसर्च का कहना है कि कुछ वर्षों में पैंतालीस फीसदी नौकरियां स्वचालित होने जा रही हैं। हाल के दिनों में प्रौद्योगिकी ने निर्णय लेना सीख लिया है।
तकनीक के विकास की गति एक दशक में कम से कम दोगुनी हो जाती है। लेकिन इसके साथ इसके बेकाबू हो जाने का डर भी उतनी ही तेजी से फैला है। गूगल और एल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने हाल में कहा भी था कि मशीनी दिमाग को लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कृत्रिम मेधा तकनीक संबंधी नियम बनाने की मांग पर जोर दिया। उनका कहना है कि हम नई तकनीक पर लगातार काम करते रह सकते हैं, लेकिन बाजार व्यवस्थाओं को उसके किसी भी तरह के इस्तेमाल की खुली छूट नहीं होनी चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब पिचाई ने कृत्रिम मेधा तकनीक के खतरों को लेकर दुनिया को आगाह किया है। इससे पहले भी साल 2018 में कंपनी के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि- ‘दुनिया पर मशीनी दिमाग का जितना असर होगा, उतना शायद ही किसी और आविष्कार का होगा। इंसान आज जिन चीजों पर काम कर रहा है, उनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण यही तकनीक है, शायद आग और बिजली जितनी ही महत्त्वपूर्ण। लेकिन ये इंसानों को मार भी सकती है। हमने आग पर काबू पाना सीख लिया है, पर इसके खतरों से भी हम जूझ रहे हैं।’
बहुत से लोग कहते हैं कि आगे चल कर इंसानों को रोबोट से खतरा होगा। यह डर बेमानी है। हालांकि जिस तरह से हम मशीनी दिमाग पर निर्भर होते जा रहे हैं, उससे खतरे तो बढ़े ही हैं। इंसान ने तकनीक की तरक्की के साथ बहुत-सी स्मार्ट मशीनें बना ली हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी मशीनों का दखल बढ़ता जा रहा है। मशीनी दिमाग हमारी कई तरह से मदद करते हैं। जैसे एपल का सीरी या माइक्रोसाफ्ट का कोर्टाना। ये दोनों हमारे निर्देश पर कई तरह के काम करते हैं। बहुत से कंप्यूटर प्रोग्राम हैं, जो कई फैसले करने में हमारी मदद करते हैं। गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी डीपमाइंड, ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस के साथ मिल कर कई परियोजना पर काम कर रही है। आजकल मशीनें शल्य क्रियाएं आपरेशन तक कर रही हैं। वे इंसान के शरीर में तमाम बीमारियों का पता लगाती हैं। मशीनी दिमागों की मदद से आज नई दवाएं तैयार की जा रही है। इसी तरह पूरी दुनिया में जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था कंप्यूटर की मदद से ही संचालित हो रही है। हवाई यातायात नियंत्रण के लिए भी इस मशीनी दिमागों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा खनन उद्योग से लेकर अंतरिक्ष तक में इस मशीनी दिमाग का इस्तेमाल, इंसान की मदद के लिए किया जा रहा है। शेयर बाजार से लेकर बीमा कंपनियां तक मशीनी दिमाग की मदद से चल रही हैं। मशीनी दिमाग वही काम करता है जो आमतौर पर बुद्धिमान लोगों के जिम्मे होते हैं। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक प्रोफेसर के मुताबिक मशीनी दिमाग कक्षा में साथ पढ़ने वाले उस साथी की तरह है जिसे काफी अच्छे नंबर मिलते हैं क्योंकि वे रट के जवाब दे देते हैं, लेकिन वे क्या बता रहे हैं, उन्हें इसकी समझ नहीं होती है। कृत्रिम मेधा तकनीक स्मार्ट फोन, कंप्यूटर आदि के जरिए हमारी जिंदगी को आसान बनाती है। ये हमें खाना, कार और दूसरी चींजें आनलाइन मंगाने और उनके लिए भुगतान करने में मदद करती है। इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब रक्षा क्षेत्र में इसका काफी इस्तेमाल होता है। साइबर सुरक्षा में भी इसका इस्तेमाल होता है।
स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े कुछ क्षेत्रों में भी मशीनी दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कैंसर, मधुमेह और अल्जाइमर का बेहतर इलाज तलाशा जा सकता है। पर मशीनी दिमाग के गलत रास्ते पर जाने का एक सार्वजनिक उदाहरण साल 2016 का ही है। तब माइक्रोसॉफ्ट ने ‘टे‘ नाम का चैटबोट ट्विटर पर रिलीज किया। कंपनी का विचार था कि लोग इसे लेकर जो ट्वीट करेंगे उसके जरिए टे स्मार्ट होता जाएगा। पर ये चैटबोट कुछ ही घंटे में ही ‘नाजी और नस्लभेदी संदेश करने लगा। तब माइक्रोसाफ्ट ने इसे हटा लिया था। इससे जाहिर होता है कि मशीनी दिमाग पर निगरानी की कितनी जरूरत होती है।
साल 2017 में टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा था कि अगर आप मशीनी दिमाग से चिंतित नहीं हैं तो आपको चिंतित होना चाहिए। ये उत्तर कोरिया से अधिक खतरनाक हैं। सोशल मीडिया पर मस्क ने जो तस्वीर पोस्ट की थी उसमें लिखा था ‘आखिर में जीत मशीनों की होगी।’ मस्क ने नेताओं से अपील की थी कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मशीनी दिमाग को काबू में लाने के लिए नियम बनाए जाएं। दुनिया को ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत समझाने वाले जाने-माने भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हाकिंग ने भी कहा था कि ‘मैं मानता हूं कि कृत्रिम मेधा तकनीक को मानवता की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इंसान को इस पर काबू करने का कोई न कोई रास्ता तलाशना पड़ेगा।’
अब उदारवाद को खलनायक साबित करने की कवायद
हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )
आज महान विचारक जॉन लॉक की 390वीं जयंती है। उनकी जयंती हम उस समय मना रहे हैं, जब उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में बहुत गहरे तक दफन करने के जतन तकरीबन पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं। जॉन लॉक की गिनती विश्व के उन दार्शनिकों में होती है, जिन्होंने राजनीति के केंद्र में उस आम आदमी को लाकर खड़ा किया, जो पहले सिर्फ शासित था। कोउ नृप होउ हमहि का हानि के फलसफे के संग जीने वाले इस आम आदमी के हाथ में न उसका वर्तमान था और न भविष्य। इन हालात में जॉन लॉक ने लोगों के अधिकार की बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का अपने जीवन पर प्राकृतिक अधिकार है। किसी ने अपनी मेहनत से जो संपदा अर्जित की है, उस पर पहला हक उसी का है, किसी सामंत या राजा-महाराजा का नहीं, यह बात सबसे पहले जॉन लॉक ने ही कही। उनकी जिस बात ने राजनीति की पूरी सोच बदल दी, वह थी- शासन वही होना चाहिए, जो जनता को स्वीकार्य हो।
अपने इन्हीं विचारों के साथ जॉन लॉक ने जिस उदारवाद की नींव रखी, वहीं से भविष्य की तमाम क्रांतियों और बड़े बदलावों के रास्ते तैयार हुए। फ्रांस की क्रांति भी इसी नींव पर खड़ी हुई और उस औद्योगिक क्रांति की इमारत भी, जिसने सभी लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करने के सपनों को आश्वासन में तब्दील कर दिया। यह उदारवाद ही था, जिसने मानव अधिकारों और नागरिक अधिकारों को सभ्यता का केंद्रीय तत्व बना दिया। अगली मंजिल लोकतंत्र था, जो पूरे मानव विकास की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जाता है। हालांकि, अब भी ये अधिकार दुनिया के कई देशों के लोगों की हसरत हैं। कुछ में तो इसे लेकर संघर्ष भी चल रहे हैं। लेकिन जहां ये सारे अधिकार हकीकत बन चुके हैं, वहां उदारवाद पर नाक-भौं सिकोड़ने का एक नया चलन शुरू हो गया है।
पिछले तकरीबन एक दशक में हम एक ऐसी दुनिया में पहंुच गए हैं, जहां उदारवाद को खलनायकत्व ओढ़ाकर उसे बहुत सारी समस्याओं की जड़ बताया जाने लगा है। यहां तक कि हर किसी को व्यवस्था में एक संभावना सौंपने वाले इस विचार को लेकर कई गालियां भी गढ़ी जाने लगी हैं। भारत में भी यही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उदारवाद को पानी पी-पीकर कोसते थे। व्लादिमीर पुतिन ने पिछले दिनों कहा था कि उदारवाद के विचार अब गुजरे जमाने की चीज होकर रह गए हैं। इस नए चलन के दर्शन हमने कनाडा में भी किए हैं, पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी, जापान, यूनान, पुर्तगाल, स्पेन और इंग्लैंड में भी। दो साल पहले प्रसिद्ध पत्रिका न्यूजवीक ने इस मसले पर एक बहस छापी थी, जिसका शीर्षक था- ‘सारा दोष जॉन लॉक पर ही मढ़ा जाए?’ अचानक यह बदलाव कैसे हो गया? जिसे भविष्य का वायुमंडल माना जा रहा था, वह कठघरे में कैसे खड़ा हो गया? बहुत सारे विद्वान इस बदलाव की थाह पाने के लिए सिर खपा रहे हैं।
अमेरिकी चिंतक फ्रांसिस फुकुयामा ने उदारवाद को लेकर दो किताबें भी लिख डाली हैं। उनका कहना है कि वैश्वीकरण के चक्कर में दुनिया ने राष्ट्रवाद से मुंह मोड़ लिया, इसलिए उदारवाद ठुकरा दिया गया। एक दूसरी आलोचना यह है कि यह विचार अपने वादों पर खरा नहीं उतर सका, इसलिए सिंहासन से उतार दिया गया। वैसे नए विचारों का सामने आना और पुराने विचारों का रुखसत हो जाना मानव इतिहास के लिए कोई नई बात नहीं है। इसलिए सदियों पुराने उदारवाद से दिल लगाने की कोई वजह नहीं है। मगर यहीं दिक्कत भी है। फिलहाल हमारे सामने न कोई नया विचार है और न ही कोई नया विमर्श। हम ऐसे मोड़ पर हैं, जहां कुछ चीजों को चुन-चुनकर खारिज किया जा रहा है, बहिष्कार हो रहा है। अमेरिका में इसे ही ‘कैंसल कल्चर’ का नाम दिया गया है। जो है उसे वर्तमान और इतिहास से हटा दो। विकल्प की चिंता किसे है?
आज 390वीं जयंती पर जॉन लॉक को कोई श्रद्धांजलि देता नहीं दिख रहा। लेकिन उनके विचारों को या उनसे शुरू हुई परंपरा को श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला चल रहा है, उसमें अच्छे भविष्य का कोई आश्वासन नहीं है। इसीलिए यह डराता भी है। यह सिलसिला और डर कहीं हमारे समय का स्थायी भाव न बन जाए, इसकी आशंका परेशान करने वाली है।
