
28-11-2022 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:28-11-22
Date:28-11-22
Pill Carefully
Hospitals, doctors, chemists – they all need a stronger push towards rational use of antibiotics
TOI Editorials
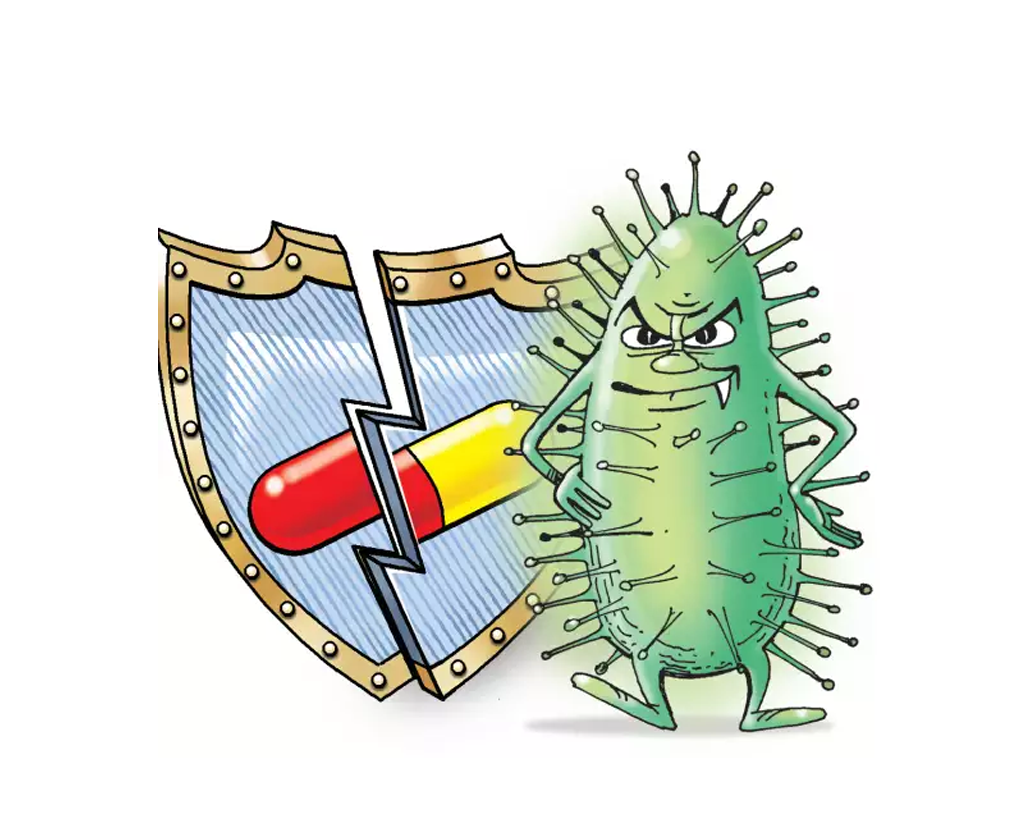
The costs of using antimicrobial prescriptions for syndrome management rather than based on a definitive diagnosis have been showing up in multiple ICMR studies of recent years. Last year’s data for example indicates that resistance to Imipenem, which is used to treat infections caused by bacteria E coli, has increased from 14% in 2016 to 36% in 2021. While the 360° reality is that such resistance is also being fed by the food industry, contaminated soil and poor sanitation, doctors and hospitals have a direct role in the matter, and they are being asked for quite a straightforward change in practice.
On the regulator’s side too, the crisis simply hasn’t been tackled as rigorously as needed. For example, instead of still being at pilot stage, stewardship programmes should by now have spread across hospitals, transparently reporting in both prevalent and targeted levels of antibiotic use. The challenge is of course made worse by how widely chemists stand in for doctors, dishing out antibiotics as blithely as if these were oranges. ICMR, CDSCO and state drug controllers all need to step up the audits and updation needed to depress antimicrobial resistance.
Shifts unexplained
System of shuffling High Court judges without consent needs reconsideration
Editorial

Transfer of judges may be needed for exchange of talent across the country and to prevent the emergence of local cliques in the judiciary. However, the power of transfer has always been seen as a possible threat to judicial independence. Even under the Collegium system, it seems it is difficult to dispel the impression that the threat of transfer hangs over every judge’s head. The Memorandum of Procedure is clear that a judge’s consent is not necessary to effect a transfer. The current norm is that all transfers ought to be in public interest, that is, for better administration of justice throughout the country. It also says the personal factors of the judge, including his preference of places, should invariably be taken into account. No one knows if these requirements are fulfilled in each case. Why a puisne judge should be shifted to another State without being made a Chief Justice is seldom explained. Usually, it sets off speculation that the reasons are either allegations against the judge or the discomfiture that his judicial orders are causing to the government. Disclosure of the actual reason may not always be possible. However, it hardly needs to be stressed that transfer cannot be used as a punitive step. The time may have come for a complete review of the provisions for transfer of High Court judges.
सामाजिक न्याय को मिला नया आयाम
अश्विनी कुमार, ( लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं )
सामान्य श्रेणी के कमजोर आर्थिक वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश में सामाजिक न्याय की मुहिम में एक मील का पत्थर है। इसके माध्यम से शीर्ष अदालत ने सवर्ण वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था को न्यायसंगत ठहराया है। इसके साथ ही इस आरक्षण से जुड़े 103वें संविधान संशोधन को लेकर ऊहापोह और भ्रम की स्थिति दूर हुई। शीर्ष अदालत ने इस संशोधन को लेकर दी जा रही ऐसी दलीलों को भी खारिज कर दिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे (केशवानंद भारती, 1973 मामले) का उल्लंघन करता है और इस कारण यह आरक्षण का आधार नहीं हो सकता। पांच सदस्यीय पीठ ने बहुमत से इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस 10 प्रतिशत आरक्षण से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की गैर-क्रीमी लेयर को बाहर रखना किसी प्रकार का भेदभाव है। इसके अतिरिक्त यह दलील भी कहीं नहीं ठहर पाई कि यह संविधान संशोधन आरक्षण पर प्रवर्तित 50 प्रतिशत की सीमा रेखा का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने संविधान संशोधन के मर्म पर बहुमत से मुहर लगाई कि आर्थिक विपन्नता और संबंधित पहलुओं का समाधान गरीबों का सशक्तीकरण करने की सरकारी अफर्मेटिव एक्शन योजनाओं का हिस्सा होना चाहिए, जो पिछड़ों के लिए जातिगत आरक्षण के दायरे में नहीं आता। पीठ में बहुमत के निर्णय के मूल भाव को अल्पमत न्यायाधीशों ने भी स्वीकार किया है कि मानवीय गरिमा पर गरीबी के घातक प्रभाव जाति-निरपेक्ष हैं। वास्तव में गरीबी जाति या कोई अन्य पहचान देखकर त्रस्त नहीं करती। स्मरण रहे कि सामाजिक-आर्थिक असमानता ने संवैधानिक प्रस्तावना को भी प्रेरित किया है और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों से लेकर मूल अधिकारों में इसकी व्याख्या भी है और यही इस मामले में भी बहुमत के फैसले का आधार बना।
संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर पीठ में बहुमत ने यही पाया कि आरक्षण समानता के सिद्धांत में एक अपवाद था, ऐसे में यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं। इस प्रकार इसे उन लोगों के लिए संशोधित किया जा सकता है, जिन्हें अभी तक इस प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया है। अदालत ने कहा कि संविधान संशोधन के अंतर्गत नए लाभार्थियों को आरक्षण के लिए एक विशिष्ट एवं अलग श्रेणी के रूप में तार्किक पृथक्करण और लक्ष्य प्राप्ति जैसी दो संवैधानिक कसौटियों के रूप में देखा जा सकता है। जहां तक आरक्षण की 50 प्रतिशत निर्धारित सीमा की बात है तो उस पर यही कहा गया कि यह एक न्यायिक संकल्पना ही थी, जिसका सरोकार केवल पिछड़े वर्गों से था और यह अवधारणा ‘भविष्य के लिए अनम्य और अचल’ भी नहीं थी। पुराने अदालती निर्णयों पर दृष्टिपात करते हुए न्यायालय ने कहा कि पूर्व में भी पिछड़ेपन की एक स्थायी श्रेणी बनाए रखने के विचार को न केवल खारिज किया गया, बल्कि यह भी स्वीकार किया गया कि देश-काल और परिस्थितियों को देखते हुए इसमें ऐसे समूहों को भी जोड़ा जा सकता है, जो सामाजिक एवं संस्थागत रूप से लाभान्वित नहीं हो पाए। गतिशील संविधान और उसमें निहित लोकतांत्रिक व्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिहाज से अदालत ने यह भी कहा कि संविधान को और अधिक जीवंत बनाने के लिए प्रत्येक पीढ़ी को अपने स्तर पर भी उसमें निवेश करना चाहिए। इस मामले में आगे जिन उदाहरणों की चर्चा की गई उनका संसदीय लोकतंत्र के लिहाज से यही सार निकलता है कि परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन साधने वाले नीतिगत विकल्प अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य हैं। इस मामले में न्यायिक स्तर पर तब तक आगे न बढ़ा जाए, जब तक कि इससे जुड़ी कोई पहल संविधान के प्रति आक्रामक न हो।
न्याय की कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया के अनुरूप आर्थिक आधार पर आरक्षण से जुड़े खंडित फैसले के बाद विधि और राजनीति के मोड़ पर जटिल सवालों को लेकर वाद-प्रतिवाद जारी रहेगा। हालांकि इस मामले में अपनी दृष्टांत महत्ता को देखते हुए बहुमत का दृष्टिकोण ही विमर्श पर हावी होगा। कानूनी बारीकियों से इतर बहुमत का फैसला संवैधानिक न्याय के विचार की विशिष्टता पर भी टिका है। साथ ही लोगों की मौजूदा संवेदनाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप और ‘तर्कसंगत जुड़ाव’ के कारण भी ऐसा प्रतीत होता है। इन सभी पहलुओं से कहीं बढ़कर बहुमत का यह फैसला आर्थिक रूप से विपन्न उस वर्ग के असंतोष को भी संबोधित करता है, जो राज्य की सशक्तीकरण नीतियों के दायरे से बाहर हो गए। इस प्रकार यह प्रतिकारात्मक अन्याय के निवारण के माध्यम से संविधान के स्थायित्व संचालन को भी प्रमाणित करता है।
इस मामले में राजनीतिक दलों ने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। हैरानी की बात है कि संसद में इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के बाद अब उनका इस पर दोहरा रवैया दिख रहा है। ऐसे दलों को यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि समझौतापरस्त सिद्धांतों से जुड़ी राजनीति को परास्त होना ही पड़ता है। उसे मात खानी पड़ती है। हालांकि, आर्थिक आधार पर आरक्षण से जुड़े अदालती फैसले में बहुमत द्वारा प्रवर्तित प्रतिपूरक भेदभाव के नए ढांचे के दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है कि विपरीत (रिवर्स) भेदभाव को उस स्तर तक भी न खींचा जाए कि वह ‘समानता के सिद्धांत को ही निगलने लग जाए।’ यह हमारे राजनेताओं की जिम्मेदारी और हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता भी है। कुल मिलाकर संवैधानिक सिद्धांत और बौद्धिक अटकलबाजी की प्रकृति में परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के उतार-चढ़ाव की स्थितियों को ही दर्शाते हैं। डा. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि ‘संविधान की आत्मा युगानुकूल है’ और आर्थिक आधार पर आरक्षण से जुड़े फैसले का अचूक संदेश उनके इसी कथन को स्मरण कराता है।
चयन पर टकराव
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच लंबे समय से खींचतान चली आ रही है। एक बार फिर केंद्रीय कानून मंत्री ने रेखांकित किया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की लिए बनी कालेजियम संविधान की मंशा के अनुरूप नहीं है। यह व्यवस्था तीस साल पहले नहीं थी, तब सरकार ही जजों की नियुक्ति किया करती थी। केंद्र सरकार फिर से वही व्यवस्था वापस लाना चाहती है। कालेजियम को लेकर बहस एक बार फिर इसलिए छिड़ गई है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में उसने क्या प्रक्रिया अपनाई है। मौजूदा केंद्र सरकार अपने पिछले कार्यकाल में ही कालेजियम व्यवस्था को समाप्त करना चाहती थी, मगर कानूनी अड़चनों की वजह से ऐसा नहीं कर पाई। हालांकि ताजा उठे विवाद के संदर्भ में प्रधान न्यायाधीश ने संविधान दिवस के मौके पर कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में कालेजियम समेत कोई भी संस्था परिपूर्ण नहीं है और इसका समाधान मौजूदा व्यवस्था के भीतर काम करना है। दरअसल, कालेजियम व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि सरकार की तरफ से की जाने वाली जजों की नियुक्ति में राजनीतिक स्वार्थ देखा जाने लगा था।
इसलिए जब मौजूदा सरकार ने कालेजियम व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव रखा, तो फिर वही तर्क सिर उठाने लगे कि अगर सरकार जजों की नियुक्ति करेगी, तो उसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने का भरोसा नहीं दिया जा सकता। कालेजियम व्यवस्था में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। इसलिए बार-बार कहा जाता है कि इस तरह उन्हें पक्षपात करने का मौका मिलता है।
उदाहरण के तौर पर कई नाम गिनाए जाते हैं, जो एक ही परिवार से चले आ रहे हैं। पिता न्यायाधीश रह चुका है, तो उसका बेटा भी जज बन जाता है। इसी तरह मित्रता और रिश्तेदारी निभाने के आरोप भी लगाए जाते हैं। हालांकि कालेजियम व्यवस्था में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में वैसी अंधेरगर्दी का उदाहरण शायद ही किसी के पास हो, जैसी सरकार द्वारा दूसरे महकमों के प्रधान का चयन करते समय देखी जाती है। ताजा प्रकरण निर्वाचन आयुक्त का है, जिसमें चौबीस घंटे के भीतर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसलिए आशंका जताई जाती रही है कि सरकार द्वारा चुने जाने वाले जजों में निष्पक्षता का अभाव हो सकता है। हालांकि उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में सरकार की भागीदारी भी होती है, पर अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए नामों में से कुछ नामों पर सरकार सहमति नहीं देती और कई बार अपेक्षाकृत कनिष्ठ को वरिष्ठता क्रम में आगे बढ़ा दिया जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय की साख अभी बनी हुई है, तो इसीलिए कि उसने खुद को काफी हद तक राजनीतिक दबावों से मुक्त रखा है। कालेजियम व्यवस्था के पक्षधर विशेषज्ञों की इस राय को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार इसलिए न्यायाधीशों को दिया गया कि वे उनकी योग्यता और प्रतिबद्धता को बहुत नजदीक से जानते हैं। बेशक उनकी नियुक्ति में परिवारवाद के कुछ उदाहरण मिल जाते हैं, पर इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी कड़े नियम-कायदे बने हुए हैं, इसलिए मनमानी नहीं हो पाती। फिर भी ताजा टकराव को देखते हुए इस विषय पर नए सिरे से और गंभीरता पूर्वक विचार की जरूरत है कि अगर जज, जजों की नियुक्ति नहीं कर सकते, तो फिर सारी नियुक्तियों को राजनीतिक दखलंदाजी से मुक्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
Date:28-11-22
पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई
प्रमोद भार्गव
मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित काप-27 जलवायु शिखर सम्मेलन में अमीर देश इस बात पर राजी हो गए हैं कि वे पृथ्वी पर बढ़े वैश्विक तापमान से हुए नुकसान की भरपाई करेंगे। अमेरिका समेत अन्य अमीर देशों ने इस जलवायु समझौते पर सहमति दे दी है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को हुए नुकसान के रूप में भुगतान करना है। इसके पहले विकसित देश इस समझौते पर चर्चा तक को राजी नहीं होते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस सम्मेलन से ही अलग कर लिया था। दरअसल, इन देशों को भय था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए उन्हें कानूनन जवाबदेह ठहराया जा सकता है। अब समझौते को लागू करने के लिए 2023 में चौबीस देशों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति तय करेगी कि अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन के लिए जो देश जिम्मेदार हैं, उनसे कितना धन लिया लाए।
इस पर्यावरण सम्मेलन में प्रतिनिधि इस बात को लेकर चिंतित थे कि एक साल पहले ग्लासगो में संपन्न हुई काप-26 में जो सहमति मीथेन गैस के उत्सर्जन पर नियंत्रण को लेकर बनी थी, उस पर उचित क्रियान्वयन नहीं हुआ। किस देश में कितनी मीथेन उत्सर्जित हो रही है, इसे नापा ही नहीं गया। मगर अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने घोषणा की है कि उपग्रहों के जरिए हर देश में मीथेन उत्सर्जन की मात्रा पर निगरानी रखी जाएगी। कार्बन डाईआक्साइड के बाद मीथेन ही ऐसी दूसरी गैस है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषक है। तापमान को वायुमंडल में रोकने के लिए यह सीओ-2 से अस्सी गुना ज्यादा सक्षम मानी जाती है। धान की खेती और पशुओं की जुगाली इसके उत्सर्जन के बड़े कारण हैं। अब तक ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं हो पाई है, जिससे इस गैस के उत्सर्जन में कमी लाई जा सके।
चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है और बड़ी मात्रा में धान की फसल उगाई जाती है, इसलिए भारत 2070 तक धान उत्पादन को प्रभावित ही नहीं करना चाहता। अगर काप-27 में हुए समझौते के मुताबिक भारत को होने वाले नुकसान का मुआवजा मिलता है, तो भविष्य में वह धान उत्पादन में कमी लाने का प्रयास कर सकता है। इसके लिए किसानों को आर्थिक मदद देनी होगी। हालांकि ग्लासगो में एक सौ तीस से अधिक देशों ने 2030 तक मीथेन के उत्सर्जन को कम करने का वादा किया था, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया।
भारत 2021 में पहली बार ‘जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक’ में शीर्ष दस देशों में शामिल हुआ था। वहीं अमेरिका सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में पहली बार शामिल था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित यूएनईपी के काप-25 में यह रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार सत्तावन उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले देशों में से इकतीस में उत्सर्जन का स्तर कम होने के रुझान दर्ज किए गए थे। इन्हीं देशों से नब्बे फीसद कार्बन का उत्सर्जन होता रहा है। इस सूचकांक ने तय किया है कि कोयले की खपत में कमी सहित कार्बन उत्सर्जन में वैश्विक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। इस सूचकांक में चीन में भी मामूली सुधार आया था, वह तीसवें स्थान पर था। जी-20 देशों में ब्रिटेन सातवें और भारत नौवें स्थान पर था, जबकि आस्ट्रेलिया इकसठ और सऊदी अरब छप्पनवें पर थे। अमेरिका खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में इसलिए आ गया था, क्योंकि उसने जलवायु परिवर्तन की खिल्ली उड़ाते हुए इस समझौते से बाहर रहने का निर्णय लिया था। इसलिए कार्बन उत्सर्जन रोकने पर उसने कोई प्रयास ही नहीं किया। अगर भारत जीवाश्म ईंधन पर दी जा रही सबसिडी को चरणबद्ध तरीके से कम करता चला जाए, तो कोयले पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी।
भारत में अब तक ऊर्जा आवश्यकताओं और पर्यावरण सरंक्षण के बीच संतुलन साधने के बावजूद कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2018 में 22.99 करोड़ टन कार्बन डाईआक्साइड पैदा हुई, जो 2017 की तुलना में 4.8 फीसद अधिक थी। भारत में इस बढ़ोत्तरी का कारण उद्योगों और विद्युत उत्पादन में कोयले का बढ़ता उपयोग था। अर्थव्यवस्था को गति देने और आबादी के लिए ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले के उपयोग पर एकाएक अंकुश लगाना मुश्किल है। लिहाजा, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत की भागीदारी सात फीसद थी, जो अब घटनी शुरू हो गई है। इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का करीब चालीस फीसद है। यह इसलिए संभव हुआ, क्योंकि एलईडी बल्ब और सौर ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया गया। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए। इससे लकड़ी के र्इंधन पर ग्रामीण भारत की निर्भरता कम हो गई। अगर कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण बना रहता है, तो भारत प्रदूषण से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई देगा। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि पिछले दिनों ग्रीनपीस की रिपोर्ट में बताया गया था कि विश्व के तीस सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में से बाईस भारत में हैं। औद्योगिक संयंत्रों और वाहनों से निकलने वाला धुआं इस प्रदूषण की मुख्य वजह हैं। हालांकि भारत जीवाश्म र्इंधन के इस्तेमाल से बचने के लिए इलेक्ट्रानिक कार, सौर और वायु ऊर्जा तथा न्यूनतम कार्बन पैदा करने वाली प्रौद्योगिकी पर लगातार जोर दे रहा है।
इटली में जी-7 की शिखर बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तब भारत और चीन पर आरोप लगाया था कि इन दोनों देशों ने विकसित देशों से अरबों डालर की मदद लेने की शर्त पर समझौते पर दस्तखत किए हैं। लिहाजा, यह समझौता अमेरिका के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाला है। यही नहीं, ट्रंप ने आगे कहा था कि भारत ने 2020 तक अपना कोयला उत्पादन दो गुना करने की अनुमति भी ले ली है। वहीं चीन ने कोयले से चलने वाले सैकड़ों बिजलीघर चालू करने की शर्त पर दस्तखत किए हैं। साफ है, यह समझौता अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने वाला है। अब ताजा रिपोर्ट से साबित हुआ है कि भारत ने कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश प्रतिबद्धता का प्रमाण दे दिया है। यहां यह भी उल्लेखनीय कि पेरिस समझौते के बाद 2015 में भारत को हरित जलवायु निधि से कुल उन्नीस हजार करोड़ रुपए की मदद मिली, जिसमें अमेरिका का हिस्सा महज छह सौ करोड़ रुपए था। ऐसे में ट्रंप का यह दावा नितांत खोखला था कि भारत को इस निधि से अमेरिका के जरिए बड़ी मदद मिल रही है।
अमेरिका में कोयले से कुल खपत की सैंतीस फीसद बिजली पैदा की जाती है। इस बिजली उत्पादन में अमेरिका विश्व में दूसरे स्थान पर है। कोयले से बिजली उत्पादन में सबसे ज्यादा ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। इस दिशा में भारत ने पचास करोड़ एलईडी बल्बों का प्रयोग किया है, जिससे कार्बन डाईआक्साइड में ग्यारह करोड़ टन की कमी लाने में सफलता मिली है। इसकी अगली कड़ी में सघन औद्योगिक इकाइयों की ऊर्जा खपत को तीन वर्षीय योजना के तहत घटाया जा रहा है। मगर अमेरिका ने कोयले की चुनौती से निपटने का अब तक कोई उपाय नहीं किया है। अमेरिका के छह सौ कोयला बिजली घरों से ये गैसें निकल कर वायुमंडल को दूषित कर रही हैं। अमेरिका की सड़कों पर इस समय पच्चीस करोड़ तीस लाख कारें दौड़ रही हैं। अगर इनमें से सोलह करोड़ साठ लाख कारें हटा ली जाती हैं, तो कार्बन डाईआक्साइड का उत्पादन सतासी करोड़ टन कम हो जाएगा।
आतंकवाद की ओर दुनिया का ध्यान खींचता भारत
कबीर तनेजा, ( शोधकर्ता, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन )
महीने भर के अंदर ही भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने में विश्व स्तर पर कमजोर पड़ते संवाद को आगे बढ़ाने के लिए दो वैश्विक मंचों की मेजबानी की है। सबसे पहले, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति की अक्तूबर में मुंबई व दिल्ली में बैठक हुई, फिर आतंक के वित्तपोषण के खिलाफ आम सहमति बनाने के लिए पिछले सप्ताह दिल्ली में सम्मेलन हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकारों को मतभेदों से ऊपर उठने और संयुक्त मोर्चा बनाकर आतंकवाद से निपटने के लिए प्रेरित किया।
पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्थितियां तेजी से बदली हैं। अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा है। जुलाई में अल-कायदा प्रमुख अल-जवाहिरी की हत्या की सार्वजनिक रूप से कम ही चर्चा हुई। आतंकवाद के खिलाफ 9/11 के बाद बनी पश्चिमी नीति की चर्चा भी थमी है। ऐसे में, आतंकवाद के खिलाफ बनी शून्यता को भारत भरना चाहता है, वह इसे केंद्रीय सुरक्षा एजेंडे के रूप में वापस लाने के प्रयास कर रहा है। वैसे, भारत के लिए ये कोशिशें नई नहीं हैं। 9/11 से पहले भी भारत सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहा था, मगर उसकी कोशिशें नाकाम होती रहीं। बहरहाल, यह सवाल बना हुआ है कि क्या अब ये प्रयास बड़े, बहुपक्षीय संगठनों पर असर डालेंगे? क्या यह आतंकवाद के खिलाफ छोटे और क्षेत्रीय संगठन बनाने की ओर बढ़ने का नया तरीका है?
वास्तव में, संयुक्त राष्ट्र में व्यवस्थागत गतिरोध ऐसे हैं, जो उसे ऐसी कोशिशों या बहसों का प्रमुख मंच बनने से रोकते हैं। हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में मुख्य वैश्विक मुद्दों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की नाकामियों की ओर इशारा किया था। वैसे, ये निराशाएं सवाल उठाती हैं कि क्या ऐसे ज्यादा व्यावहारिक और कारगर अंतरराष्ट्रीय मंच हैं, जहां आतंकवाद के खिलाफ पुख्ता प्रतिक्रिया की जा सकती है? शायद जवाब अंतर-क्षेत्रीय मंचों में निहित हो सकता है। मसलन, दक्षिण एशिया में आतंकवाद के खिलाफ कोई भी क्षेत्रीय पहल या मंच नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जैसे मंच भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता के चलते ठंडे बस्ते में चले गए हैं। ध्यान रहे, इस्लामिक स्टेट (आईएस) के समर्थकों द्वारा किए गए दो सबसे महत्वपूर्ण आतंकी हमले बांग्लादेश (2016) और श्रीलंका (2019) में हुए थे। मध्य एशियाई सरकारों के बीच ऐसी ही कई वार्ताओं के विपरीत तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी पर भी दक्षिण एशिया में कोई वार्ता नहीं हुई है। नई दिल्ली के नजरिये से देखें, तो वह पाकिस्तान को छोड़कर अपने अन्य पड़ोसियों को भी सार्वजनिक रूप से साथ नहीं लेती है, यह बिल्कुल वैसा ही है, मानो कूटनीतिक ताश की गड्डी से इक्का ही गायब हो।
ईरान, इजरायल जैसे देश भी तीखी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद क्षेत्रीय संवाद को महत्व देते हैं। इजरायल ने 2020 में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर से पहले कई अरब राज्यों के साथ परदे के पीछे संवाद किया था। हाल ही में, सऊदी अरब व ईरान ने बड़े पैमाने पर संघर्ष की आशंका को कम करने के लिए वार्ता की है। समाधान के ये क्षेत्रीय प्रयास हमेशा काम नहीं कर सकते, पर ज्यादा जटिल क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने में कारगर तो हो ही सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर ऐसी वार्ता पसंदीदा तरीका बनती जा रही है।
अफगानिस्तान की घटनाओं से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का भविष्य बाधित हो गया है। तालिबान के साथ समझौता करने वाले अमेरिका ने कई गैर-राज्य उग्रवादी समूहों के लिए भी संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। यूरोप के सबसे वांछित अपराधियों में से एक पूर्व अल-कायदा सहयोगी हयात तहरीर को सीरिया में गिरफ्तार करना और इटली भेजना, कुछ आतंकी समूहों और पश्चिम के बीच जुड़ाव के नए स्तर को दर्शाता है।
ऐसे में, भारत ने वैश्विक सुर्खियों से दूर हो रहे मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचकर अच्छा किया है। हालांकि, काफी कुछ वैश्विक समुदाय को प्रेरित करने की भारत की क्षमता पर निर्भर करेगा। इसी से आतंकवाद विरोधी ढांचा तैयार करने की विश्वव्यापी प्रतिक्रिया तय होगी।