
26-04-2022 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:26-04-22
Date:26-04-22
Plotting Progress
Political risks of land acquisition are borne by states. They need better incentives
TOI Editorials
The national monetisation pipeline has identified 25 airports run by the Airports Authority of India (AAI) for action over the next three years. Four of them are located in Tamil Nadu – all international airports. GoI’s airport monetisation plan needs to be studied with the TN government’s major industries policy note, 2022-23, to see how the approach can be tweaked to realign incentives between the two levels of government to encourage industrial development. It’s essential because the current airport infrastructure policy doesn’t reconcile political risks to potential rewards of monetisation.
TN’s policy note is an extension of what the previous DMK government suggested during the UPA-1 era. The note says that land forms the major portion of overall project cost. Henceforth, if the state transfers land free to GoI, which subsequently monetises the infrastructure, the state should be entitled to a share of the gains. It’s a sensible suggestion and one GoI should consider. Revenue from infrastructure flows to governments through two streams. One, through taxes, which are split between GoI and states on the basis of the Finance Commission’s recommendations and GST Council’s decisions. Two, through subsequent monetisation of an asset.
It’s the second stream that needs fine-tuning. Often, land is obtained by invoking a legislation to forcibly take over privately-owned property to serve a public purpose. This can sometimes extract a political cost that’s borne entirely by the state government. This risk can be mitigated by giving states a share of the upside arising out of monetisation. A mismatch between risk and reward across the two levels of government has acted as a drag on India’s industrialisation. The UP government’s example is pertinent here. It holds the equity of Noida International Airport incorporated in 2018. After overseeing the land acquisition process, it contracted Zurich Airport to build the airport and then operate it for 40 years. The upside of a potential monetisation will accrue to UP. True, Jewar is a greenfield project and AAI’s are existing airports. But the principle holds.
Separately, there’s a need to re-evaluate mechanisms of awarding compensation when land is acquired. The legislative process is complex and tilts towards the state. Sometimes this results in paltry compensation. On paper, there are redressal mechanisms. However, it’s almost impossible for an individual to get redress. Tweaks in laws allowing acquisition can help mitigate resistance to acquisition. The doctrine of eminent domain needs to be balanced with fairness.
Date:26-04-22
Retire Judges Later
Constitutional court judges are being pensioned off too early. Their services are badly needed
TOI Editorials

The vacancy problem is more pronounced in HCs where 45% of pending 59 lakh cases are awaiting disposal for over five years. While the overall vacancy position is 35% in HCs, in big HCs like Allahabad, Calcutta and Patna nearly 50% sanctioned posts lie vacant. The bizarrely different retirement ages for SC-HC judges may be a colonial legacy, but the UK has progressively increased retirement age for judicial office holders to 75. The benefits of India following suit go beyond pendency.
It’s no one’s case that judges turn unfit after 62 or 65. Many secure positions as judicial members of tribunals and commissions. But the hankering for post-retirement jobs weakens judicial independence vis-à-vis central and state executives. If judges serve till 70 there’s minimal incentive to seek post-retirement sinecures. Alternatively, a higher retirement age can also attract the best minds to the vocation. Only a few like Justice Rohinton Nariman and Justice UU Lalit have left behind lucrative practices to join SC. HC collegiums also face great difficulty attracting noted lawyers because of the low retirement age of 62 and delayed appointments. Even Article 224A’s option of allowing reappointment of retired HC judges hasn’t been exercised. A fully staffed judiciary will help crores of citizens awaiting justice in civil and criminal matters.
सरकार का अंपायर के रोल में रहना बेहतर
शेखर गुप्ता, ( एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’ )
राजधानी के जहांगीरपुरी क्षेत्र में दंगों के बाद बुलडोजर और ध्वस्तीकरण अभियान फिर सुर्खियों में है, जहां उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने खासकर मुस्लिमों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को निशाना बनाया। बचाव में तर्क ये दिया कि केवल अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजधानी में डिमॉलिशन मैन- जो 1992 से 1995 के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण के आयुक्त (भूमि) पद पर सेवारत थे- के तौर पर ख्यात रहे के.जे. अल्फोंस ने बातचीत में कहा था कि ध्वस्तीकरण अभियान तभी प्रभावी होते हैं, जब पहले कुलीन वर्ग के अवैध कब्जों को निशाना बनाया जाए। वे बताते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एकाध ही अलग-थलग बसी झुग्गी-बस्ती ध्वस्त की थी।
इसने मुझे 1999 के अपने उस लेख की याद दिला दी, जो मैंने उस समय लिखा था जब न्यायपालिका अतिक्रमणों पर संज्ञान ले रही थी। यह फिर प्रासंगिक हो गया है क्योंकि सामाजिक-आर्थिक ढांचे में निचले पायदान पर रहने वालों को निशाना बनाया जा रहा है और अमीर और ताकतवर लोगों को हमेशा की तरह खुली छूट मिली हुई है। लेकिन इस स्तंभकार जैसा कोई मुक्त-बाजार का हिमायती शिकायत क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें सरकार की जरूरत है। दरअसल, लाइसेंस-कोटा राज की तुलना में एक मुक्त बाजार, नियंत्रण मुक्त और उपभोक्ताओं को राजा मानने वाली समृद्ध अर्थव्यवस्था में तो सुशासन की आवश्यकता अधिक होती है। क्या कभी सोचा है कि हमारे मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग, कुछ अतिरिक्त आय और इसलिए थोड़ी बचत कर पाने वाले लोग आर्थिक सुधारों को लेकर नाक-भौं क्यों सिकोड़ते हैं? एक हालिया सर्वेक्षण ने यह क्यों दिखाया कि हमारे 70 फीसदी युवा संरक्षणवाद के पक्ष में हैं? हर्षद मेहता उनकी नजर में क्या है? बहुत अधिक रेग्युलेशन का नतीजा या बहुत कम का? या फिर 1993-94 में बाजार में शुरुआती उछाल के दौरान रातोंरात उभरी सैकड़ों निजी कंपनियों की घटना का, जिसने आईपीओ के जरिए पेंशनभोगियों और वेतनभोगियों से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए, और फिर गायब हो गया? यदि डिरेग्युलेशन का नतीजा इस तरह के झांसे के तौर पर ही सामने आता है तो क्या पुराने माई-बाप सरकार वाले दिन ज्यादा बेहतर नहीं थे, जब उद्योग भवन के बाबू लाइसेंस पर कुंडली मारे बैठे रहते थे और शेयर से जुड़े पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रण उनके हाथ में होता था? लेकिन नॉन-गवर्नेंस को डिरेग्युलेशन मान लेना खतरनाक है। कोई भी मुक्त बाजार अच्छी सरकार और मजबूत कानूनों के बिना सफल नहीं हो सकता।
एक मुक्त बाजार को सरकार-संचालित अर्थव्यवस्था से भी अधिक कानूनों की आवश्यकता होती है। कानून अच्छे और निष्पक्ष होने चाहिए, लागू करने के लिहाज से डिरेग्युलेटरी होने चाहिए, और फिर इन पर अमल और निगरानी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि बाजार अपने आप में जवाबदेही की गारंटी होता तो सबसे सफल मुक्त अर्थव्यवस्थाओं में इस तरह के मजबूत नियामक तंत्र नहीं होते। बाजार, कानून और सरकारें मिलकर जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। हमारे मंत्री, वित्त सचिव, सीबीआई प्रमुख और यहां तक कि सेबी के मुखिया भी इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे पैसे लेकर गायब हुई कंपनियों के प्रमोटरों का पता लगाना और उन्हें दंडित करना मुश्किल है। सीधा सवाल यह है कि देश के शीर्ष बैंकों और वित्तीय संस्थानों की तरफ से चलाई जा रही मूल्यांकन एजेंसियों के प्रभारी अधिकारियों को क्यों नहीं पकड़ा जाता, जिनके प्रमाणपत्र प्रमोटर बड़े गर्व से लहराते घूमते थे? हम तो इसलिए ठगे गए न, क्योंकि हमने सोचा था कि इनका मूल्यांकन सम्मानित संस्थानों ने किया है।
दूरसंचार क्षेत्र में जारी तमाशा यह समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे हमने डिरेग्युलेशन को नो-रेग्युलेशन समझने की भूल कर दी है। सेवाएं बेहतर हुई हैं, अभूतपूर्व रूप से सस्ती भी हैं और इस सबका श्रेय निजीकरण को दिया जाना भी सही लगता है। लेकिन इस सबके बीच ट्राई की भूमिका के बारे में सोचें, जिससे निजी ऑपरेटर्स के साथ-साथ पुराने खिलाड़ी एमटीएनएल और डीओटी भी चिढ़ते हैं। वे टैरिफ घटाते रहते हैं और कोई गलती दिखने पर अंपायर की तरह सीटी भी बजाते हैं। अंपायरों को तो कोई भी पसंद नहीं करता लेकिन आप उनके बिना खेल भी नहीं खेल सकते। हमें सरकार की जरूरत है या नहीं, यह बहस पुराने भारतीय ताने-बाने में ही उलझी है, जहां हम किसी चीज से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आगे-पीछे सब भुला देते हैं। हम चुनाव अभियानों, मतदान, धांधली और परिणामों में इस कदर उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं यह सब किसलिए है।
मुझे कई साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह के साथ हुई बातचीत याद है, जब वे वित्त मंत्री थे। वे अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की स्थिति पर चिंतित थे। उन्होंने कहा, ‘हमारा तब तक कोई भविष्य नहीं है, जब तक हम अपने लोगों को उन सेवाओं के लिए उचित शुल्क के भुगतान के लिए राजी नहीं कर लेते जो सरकार उन्हें प्रदान करती है- जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा आदि।’ लेकिन ऐसी सरकारें हमें इसके लिए कैसे राजी कर सकती हैं, जो दूसरों को मुफ्त बिजली की लूट, बिना टिकट यात्रा, नियमों-कायदों की धज्जियां उड़ाने और अवैध निर्माण करने की अनुमति देती हैं, वहीं अधिकारी हाउस टैक्स के लिए हमें परेशान करते रहते हैं और पूरी तरह से कानूनी कॉलोनियों में हमारी कथित तौर पर बड़ी बालकनी ध्वस्त करने में जरा भी देर नहीं लगाते हैं?
Date:26-04-22
नागरिक से ज्यादा उपभोक्ता बनने की कोशिशों से हानि
नंदितेश निलय, ( लेखक और वक्ता )
रूस -यूक्रेन युद्ध में अभी तक दोनों तरफ से हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और अगर हम यूएन की रिपोर्ट को मानें तो 3 मिलियन से ज्यादा लोग घर छोड़कर इधर-उधर शरण ले रहे हैं। तो क्या महामारी के वक्त भी हिंसा ही मनुष्य की बुद्धि का साधन और साध्य है? और यह भी हिंसा से कम नहीं है कि विश्व स्तर पर शांति का न कोई दूत है और न वो जनमानस। युद्ध 24 फरवरी को शुरू हुआ और बस चल ही रहा है। ऐसा नहीं लगता कि पूरे विश्व को फिर से महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को अपनाने की जरूरत है?
8 फरवरी 1922 को, एक हिंसक भीड़ ने चौरी-चौरा में इमारत में आग लगा दी, जहां 22 पुलिस अधिकारी थे। उस समय गृह सचिव ने कहा, यह राज के खिलाफ विद्रोह है। लेकिन महात्मा गांधी के लिए, यह हिंसा ही थी। यहां तक कि उन्होंने हिंसा के लिए आत्म-दंड के रूप में पांच दिनों का उपवास भी किया। वे अहिंसा के साधनों के साथ प्रयोग कर रहे थे, और उनके लिए साधन उतने ही आवश्यक थे जितने कि साध्य। उनके लिए किसी भी प्रकार की हिंसा का तरीका अस्वीकार्य था। महात्मा गांधी के अनुसार, अहिंसा हमारी प्रजाति का कानून है क्योंकि हिंसा जानवर का कानून है। ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती है। यह एक अदम्य इच्छाशक्ति से आती है।
गांधी विश्व-व्यवस्था में विश्वास करते थे, जहां साध्य की खोज में साधनों का समान महत्व होगा। मानव-विकास को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कभी भी साधनों से समझौता नहीं किया। जब हम पिछले सत्तर वर्षों के भारत को देखते हैं तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि सर्वोत्तम इरादों के बावजूद कई बार हमने नागरिक से ज्यादा उपभोक्ता बनने की कोशिश की है। उपभोक्तावाद की ऊंची आकांक्षाओं ने नागरिकता के मूल्यों को ढक दिया है। इसने हमें तनावग्रस्त और क्रोधित बना दिया है। आजकल छोटी-छोटी दलीलें भी हिंसक हो जाती हैं। हम क्या विकसित देश के नागरिक भी बात-बात पर हिंसक हो रहे हैं। चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या हॉलीवुड के कलाकार। क्रोध तो मानो पहला परिचय हो गया है। लोग एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि गांधी ने अहिंसा के माध्यम से दुनिया को माना और प्रबुद्ध किया।
गांधी ऐसे नेता थे जिन्होंने अलगाव और उदासीनता का दर्द महसूस किया। गांधी को याद करना शब्दों से नहीं कर्मों में हो सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता गुन्नार मायर्डल ने विशेष रूप से कहा था कि भारत इतनी सारी परेशानियों के बीच में है और अधिकांश मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है यदि हम गांधी के मार्ग को नहीं भूले होते। इसलिए संस्थाओं को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने साधनों का चयन करते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। उन साधनों को मानव जाति की एकता, प्रेम, सम्मान, सच्चाई और सेवा की भावना की अपनी दृष्टि प्रस्तुत करनी चाहिए। वे एक सामाजिक व्यवस्था में विश्वास करते थे, जो अहिंसक और न्यायपूर्ण है।
आज युद्ध में फंसे विश्व के लिए गांधी की अहमियत और बढ़ गई है, उस अहिंसा और सद्भाव की। भगत सिंह ने अपने पिता किशन सिंह के साथ आखिरी बातचीत में एक जोरदार अपील की थी कि आपको अपने जनरल (गांधी) का समर्थन करना चाहिए। तभी आप देश के लिए आजादी हासिल कर पाएंगे। रोमां रोलां ने भी उल्लेख किया है कि बड़ी संख्या में सभा में गांधी को उनकी मृदु आवाज के कारण नहीं सुना जा सकता था, लेकिन फिर भी, लोग उनकी बात सुनते थे और वह केवल उनके हावभाव से। लेकिन शायद विश्व भी उनको सुने उन बमों के धमाकों से पहले। और सत्य की प्रयोगशाला में इस महामारी के वैक्सीन को ढूंढे ना कि कोई और हिंसा के साधन। वे ही देश फिर से भारत की ओर देखेंगे और उन गांधीवादी मूल्यों को याद करेंगे जहां साध्य ही साधन और साधन ही साध्य हो जाता है।
समान नागरिक अधिकारों की प्रतीक्षा
प्रो. हरबंश दीक्षित, ( लेखक विधि मामलों के विशेषज्ञ एवं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज के सदस्य हैं )
सभी वर्गो के लिए एक जैसे सिविल कानून यानी समान नागरिक संहिता एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस संहिता के निर्माण की बात कही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि अब समान नागरिक संहिता की बारी है। यद्यपि हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से पहले ही अपनी भावना व्यक्त कर दी थी, किंतु पिछले 72 वषों से कोई ठोस कदम नही उठाया जा सका। यह अनुच्छेद 44 सबसे अधिक दुष्प्रचारित हिस्सों में से एक है। इस उपबंध के साथ बहुत अन्याय हुआ है। इसमें देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात कही गई और सरकार से अपेक्षा की गई कि वह पंथ, जाति, क्षेत्र, भाषा जैसे बंटवारा करने वाले आधारों की परवाह किए बगैर सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए, जो मानवीय गरिमा का सम्मान करता हो और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उतरता हो। दुर्भाग्यवश इस पवित्र भावना को आगे बढ़ाने के बजाय हमारे अधिकतर नेताओं ने अपनी फितरत के मुताबिक एक हौआ खड़ा कर दिया और इस विषय पर तार्किक बहस करने के बजाय उसे सांप्रदायिक रूप देकर अछूत बना दिया। इस मामले में हम लोकशाही की महान पंरपराओं से भी मुंह चुराते दिखे। कुछ लोग इस विषय पर स्वस्थ बहस करने के बजाय इसके प्रस्तावकों को तब तक लानत भेजते रहते हैं, जब तक वह थक हार कर बैठ न जाए।
हमारे देश में अधिकतर मामलों में एक जैसा कानून लागू होता है। जमीन का क्रय-विक्रय, किरायेदारी और अन्य दीवानी मामलों में पहले से ही एक जैसा कानून है, लेकिन विवाह, उत्तराधिकार, वसीयत, दतक ग्रहण जैसे मामलों में आजादी के पहले से ही अलग-अलग संप्रदायों के लिए अलग कानून रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि विवाह और भरण-पोषण से जुड़े मामलों का संबंध किसी उपासना पद्धति से नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा से है। यदि संतानहीन व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी वंश परंपरा आगे बढ़ाना चाहता है या उससे उसे सुरक्षा बोध का अहसास होता है, तो इससे किसी उपासना पद्धति की अवमानना कैसे हो सकती है? यदि किसी कानून से किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने के बाद उसके लिए गुजारा भत्ते की व्यवस्था कर दी जाती है तो इसमें मत-मजहब क्यों आड़े आना चाहिए? यदि वैवाहिक संबंधों में समानता सुनिश्चित की जाती है तो इस पर किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है?
आजादी के बाद समानता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक हिंदू विधि में व्यापक परिवर्तन किए गए। पहले हिंदू समाज के पुरुष एक से अधिक शादियां कर सकते थे। हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया। पति-पत्नी को विवाह विच्छेद करके सम्मानपूर्वक एक-दूसरे से अलग रहने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार दिया गया। पिता की संपत्ति में बेटियों को भी अधिकार देने की परंपरा शुरू हुई। गोद लेने के मामलों में भी पति के एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। इनमें कुछ सुधार दूसरे संप्रदायों में पहले से ही थे। मसलन ईसाई समाज में पुरुष एक ही शादी कर सकता था। हिंदू कोड बिल के माध्यम से पारंपरिक विधि की जगह मानवाधिकारों और समानता के सिद्धांतों को तरजीह दी गई, लेकिन वोट बैंक के कारण दूसरे समुदायों में ऐसा नहीं हो सका। आधुनिक सोच का लाभ समाज के केवल एक वर्ग तक ही सीमित न रहे, अपितु वह सभी समुदायों को भी हासिल हो, इसके लिए अदालतें समान नागरिक संहिता के निर्माण के लिए लगातार कोशिश करती रही हैं। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह खेद का विषय है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में तय की गई राज्य की जिम्मेदारी अब निर्जीव शब्द समूहों का संग्रह मात्र बन कर रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा शाहबानो को गुजर-बसर के लिए महज कुछ धनराशि तय की थी, लेकिन इसे मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी के रूप में प्रचारित किया गया। कुछ लोगों ने इस फैसले को पूरी कौम की अस्मिता पर खतरा करार कर दिया। राजीव गांधी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार भी इस वाग्जाल की आंधी का सामना नहीं कर सकी। उसे झुकना पड़ा और कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को गुजारे भत्ते के अधिकार से वंचित करना पड़ा। यह मुस्लिम महिलाओं की अनदेखी ही नहीं, उनके साथ किया जाने वाला घोर अन्याय भी था। इससे संविधान की पराजय हुई और मानवता एवं समानता के सिद्धांतों की हेठी हुई। इससे यह भी संदेश गया कि अब समान नागरिक संहिता के लिए पहल मत करना। बाद के घटनाक्रम बताते हैं कि तार्किक विचारधारा के लोग अपनी बात कहते रहे और सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करता रहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
शाहबानो प्रकरण के बाद सरला मुदगल और लिली थामस जैसे कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता न होने के दोषों को उजागर करते हुए उस पर अमल का निर्देश दिया। खुद मुस्लिम समाज के विद्वानों मुहम्मद करीम छागला, प्रो. ताहिर महमूद, एमयू बेग आदि ने समान नागरिक संहिता की कमी की ओर बार-बार इशारा किया, लेकिन हमारे राजनीतिक नेतृत्व पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। संसद में इस पर ढंग से बहस भी नहीं हो सकी। कम से कम अब तो समाज के व्यापक हित को देखते हुए सभी पंथनिरपेक्ष हितचिंतकों को आगे बढ़कर समान नागरिक संहिता की दिशा में पहल करनी चाहिए और यह पहल भी ऐसी होनी चाहिए जो किसी निर्णय पर पहुंचे ताकि हम एक प्रगतिशील समाज के रूप में एकजुट हो सकें। इससे हम संवैधानिक आदर्शो की स्थापना में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे।
 Date:26-04-22
Date:26-04-22
नीतिगत मदद
संपादकीय
गत सप्ताह राजीव कुमार के इस्तीफा देने के बाद अर्थशास्त्री सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसी संस्थान में ऐसे बदलाव हमेशा इस बात का अच्छा अवसर होते हैं कि वह अपनी स्थिति की समीक्षा करे तथा स्वयं को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए जरूरी बदलाव लाए। यह बात निजी उपक्रमों और सरकारी विभागों दोनों के लिए सही है। नीति आयोग के मामले में यह बात खासतौर पर प्रासंगिक है क्योंकि यह अभी भी अपेक्षाकृत नया संस्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले भाषण में यह घोषणा की थी कि योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना ने योजना निर्माण के एक युग का अंत किया और भारत पंचवर्षीय योजनाओं से आगे निकला।
विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर आशंका थी कि यह नया संस्थान जो कि एक सरकारी थिंक टैंक है, क्या हासिल करेगा। सात वर्षों के बाद यह कहना सही होगा कि कई पहलों के साथ इसने सरकारी पारिस्थितिकी में अपनी जगह बना ली है। बहरहाल तेजी से बदलते आर्थिक माहौल में उससे और अधिक काम करने की अपेक्षा है। इसके बुनियादी लक्ष्य, जैसा कि नीति आयोग स्वयं कहता है, ‘राज्यों की सक्रिय सहभागिता के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और नीतियों को लेकर साझा दृष्टि विकसित करना।’ उससे यह भी अपेक्षा है कि वह इस दृष्टिकोण के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देगा कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। उसने इस क्षेत्र में काम किया है और कई नीतिगत दस्तावेज तथा रैंकिंग तैयार की हैं जो प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने में मदद करती है। राज्य यह देख सकते हैं कि वे कहां पिछड़ रहे हैं और अन्य राज्यों की बेहतर बातों को अमल में ला सकते हैं। केंद्र सरकार ने उसकी कई अनुशंसाओं को अपनाया है। उदाहरण के लिए नीति आयोग ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाई। नए नेतृत्व के अधीन आगे बढ़ते हुए नीति आयोग के लिए बेहतर होगा कि वह कुछ व्यापक क्षेत्रों पर नजर डाले और कुछ ऐसा करे जो उसके अब तक के कामों से अलग हो। भारत ने योजना निर्माण को त्याग दिया है लेकिन उसे मध्यम अवधि के नीतिगत खाके की आवश्यकता है। कोविड के कारण लगे झटके के बाद यह बात ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो गई है। महामारी ने देश की उत्पादक क्षमता को जो क्षति पहुंचाई है उसका अहसास होना बहुत जरूरी है। वृद्धि अनुमान से संकेत मिलता है कि आधार प्रभाव के समाप्त होने के साथ भारत महामारी के पहले वाले वृद्धि स्तर पर लौट जाएगा जो हर मानक से कम है। ऐसे में यह जानना अहम है कि मध्यम अवधि में सतत उच्चवृद्धि कैसे हासिल होगी। मध्यम अवधि का नीतिगत विश्लेषण तथा खाका इसमें मददगार होगा। उदाहरण के लिए नीति आयोग 2017 में प्रकाशित तीन वर्षीय योजना एजेंडे को दोबारा शुरू कर सकती है। बल्कि वह वार्षिक तौर पर ऐसे दस्तावेज पर काम कर सकती है और वर्ष भर में हुई प्रगति का आकलन कर सकती है। इससे न केवल नीतियों को लेकर व्यापक दिशा मिलेगी बल्कि बेहतर क्रियान्वयन भी संभव होगा। इतना ही नहीं सहकारी संघवाद की दिशा में भी काफी कुछ करने की आवश्यकता है। इसे ऐसा मंच बनना चाहिए जहां राज्यों के विकास संबंधी सभी मुद्दों पर चर्चा की जाए और उन्हें हल किया जाए। केंद्र में नीति आयोग के साथ राज्यों का निरंतर संवाद जलवायु परिवर्तन के एजेंडे को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगा। उसे अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र को समझने में मदद करनी चाहिए। वैश्विक आर्थिक माहौल तेजी से बदल रहा है और भारत को समुचित प्रतिक्रिया के लिए बेहतर समझ की जरूरत है। भारत अब भले सीमित व्यापार समझौते कर रहा है लेकिन कुल मिलाकर वह वैश्विक स्तर से पीछे है। व्यापक स्तर पर नीति आयोग को उचित नीतिगत हस्तक्षेप में सरकार की मदद करने के लिए और अधिक क्षमता विकसित करनी होगी।
अभी और कोशिश की जरूरत
अवधेश कुमार
अप्रैल 24 को पंचायत दिवस आया गया जैसा हो गया। अगर नरेन्द्र मोदी सरकारी इस दिवस पर पंचायतों के लिए पुरस्कारों की घोषणा न करें तो किसी को याद भी नहीं होगा कि पंचायत दिवस कब आता है। जब पी वी नरसिंह राव सरकार ने 24 फरवरी, 1992 को संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज कानून पारित किया तथा इसके एक वर्ष बाद लागू हुआ तो इसे स्थानीय स्वशासन प्रणाली की दृष्टि से लोकतांत्रिक अहिंसक क्रांति नाम दिया गया।
वास्तव में आजाद भारत की सबसे बड़ी विडंबना थी कि महात्मा गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन का अपना नेता घोषित करने के बावजूद आजादी के बाद शासन में आई सरकार ने ग्राम स्वराज के उनके सपने को संविधान के तहत अनिवार्य रूप से संपूर्ण राष्ट्र में साकार करने का कदम नहीं उठाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में ही 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने जिस त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की उसके अनुसार गांव में ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद को तभी संविधान का अनिवार्य भाग बना दिया जाना चाहिए था। उसने विकेंद्रित लोकतंत्र शब्द भी प्रयोग किया। हालांकि सभी सरकारों ने भारत में ग्राम पंचायतों को सशक्त करने की वकालत की, अलग-अलग राज्यों में थोड़े-बहुत अंतर के साथ पंचायती ढांचा कायम हुए पर इसे व्यापक और समग्र संवैधानिक ढांचागत स्वरूप 1992 के संशोधन द्वारा ही प्राप्त हुआ।
ध्यान रखिए, स्वतंत्रता के बाद संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघ, समवर्ती और राज्य सूची के आधार पर ही किया गया, जिनमें पंचायतों को अधिकार नहीं मिल सका। 1992 का संशोधन ही था, जिसके तहत पंचायतों को कुल 29 विषयों पर काम करने का संवैधानिक अधिकार मिला। इस व्यवस्था ने 29 वर्ष पूरा कर 30वें वर्ष में प्रवेश किया है और संविधान संशोधन की दृष्टि से देखें तो 30 वर्ष पूरा हो चुका है। किसी भी व्यवस्था के मूल्यांकन के लिए इतना समय प्राप्त होता है। प्रश्न है कि क्या हम पंचायत प्रणाली की वर्तमान स्थिति को संतोषजनक मान सकते हैं? आज दुनिया के विकसित देश औपचारिक रूप से यह मानने को विवश हैं कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में पंचायती राज्य के माध्यम से सत्ता को नीचे तक पहुंचाने का काम अद्भुत है। सच यह है कि विश्व में सबसे ज्यादा शोध यदि किसी एक प्रणाली पर हुआ है तो वह है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था। हमें अपने देश में भले यह सामान्य काम लगे, लेकिन विश्व के लिए यह अद्भुत है। इस आधार पर स्वाभाविक निष्कर्ष यही निकलेगा कि अगर विश्व में इस व्यवस्था ने धाक जमाई है तो निश्चित रूप से सफल है। जाति और लिंग के आधार पर सत्ता में भागीदारी की दृष्टि से विचार करें तो इसने समानता के सिद्धांत को साकार किया है। 1992 के संशोधन में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण था जिसे बाद में 50 फीसद कर दिया गया। यानी इस समय करीब 2.6 लाख ग्राम पंचायतों में आरक्षण के अनुसार सत्ता की आधी बागडोर महिलाओं के हाथों में है। दूसरे, दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या 80 फीसद से ज्यादा मानी जा रही है।
विधानसभाओं एवं लोक सभा में अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अति पिछड़ी जातियों के सांसदों और विधायकों के निर्वाचित होने से जमीनी स्तर पर सामाजिक असमानता में अपेक्षित अंतर नहीं आया, लेकिन पंचायतों में इनके निर्वाचन से व्यापक अंतर आया है। एक समय स्वयं को उपेक्षित माने जाने वाला वर्ग अब गांवों और मोहल्ले में फैसले करते हैं तथा ऊंची जाति की मानसिकता में जीने वाले ने लगभग इसे स्वीकार कर समन्वय स्थापित किया है। आप किसी जाति के हों, काम के लिए ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य के घर जाना होता है। वह चाहे किसी जाति का हो उसके दरवाजे पर बैठना है। इन सब से ऊंच-नीच की मानसिकता बदल रही है। इस तरह कहा जा सकता है कि पंचायती राज में सामाजिक समानता को मनोवैज्ञानिक स्तर पर स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाया है। हां, महिलाओं के मामले में अभी यह लक्ष्य प्राप्त होना शेष है। ज्यादातर जगह निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति व्यवहार में ज्यादा सक्रिय हैं और मुख्य भूमिका उनकी होती है। किंतु अनेक जगह महिलाएं स्वयं भी सक्रिय हैं। पुरुषों और स्त्रियों के बीच राजनीतिक मामलों में बहस व विमर्श की वर्षो से कायम दूरियां घटी हैं।
चुनाव के समय आप गांव में महिलाओं के बीच भी राजनीतिक बहस होते देख सकते हैं। पढ़े-लिखे युवाओं में भी निर्वाचित होकर काम करने की ललक बढ़ी है। चुनाव आधारित लोकतांत्रिक प्रणाली की दृष्टि से देखें तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत सतत जागरूकता का साकार होना है। किंतु यह सब एक पक्ष है। इसके दूसरे पक्ष चिंताजनक और कई मायनों में डरावने हैं। सत्ता यदि शक्ति, संपत्ति और प्रभाव स्थापना का कारक बन जाए तो वह हर प्रकार की मानवीय विकृति का शिकार होता है। हालांकि लोक सभा और विधानसभाओं के अनुरूप शक्ति का विकेंद्रीकरण तुलनात्मक रूप से पंचायती राज में काफी कम है। बावजूद पंचायती राज के तीनों स्तरों के अधिकार और कार्य विस्तार के साथ जितने काम आए और उसके अनुरूप संसाधनों में बढ़ोतरी हुई उसी अनुरूप इनके पदों पर निर्वाचित होने की लालसा भी बढ़ी। वर्तमान वोटिंग प्रणाली अनेक प्रकार के भ्रष्ट आचरण की जननी है।
आज पंचायतों की चुनाव प्रणाली हर सारे भ्रष्ट व्यवहारों की गिरफ्त में आ चुका है। प्रशासन के लिए पंचायतों का चुनाव कराना विधानसभाओं और लोक सभा चुनाव से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। पंचायत प्रमुख एवं जिला परिषद अध्यक्ष आदि के चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों की बोली लगती है। समय की मांग पूरी राजनीतिक व्यवस्था की गहरी समीक्षा और उसके अनुरूप व्यापक संशोधन और परिवर्तन का है। गांधीजी ने भारत की प्राचीन प्रणाली के अनुरूप मतदान की अति सामान्य व्यवस्था दी थी, लेकिन उनके विचार के केंद्र में परस्पर एक दूसरे का हित चाहने वाला नैतिक और जिम्मेदार व्यक्ति है। तो व्यवस्था में बदलाव की कल्पना के साथ समाज में ऐसे व्यक्तियों का बहुतायत कैसे हो इस पर काम करने की आवश्यकता है।
Date:26-04-22
राष्ट्रीय भाषा नीति बने
अजीत दुबे
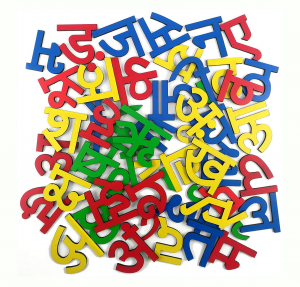
सर्वविदित है कि मातृ भाषा में ज्ञान प्राप्त करना सुगम होता है यूनेस्को ने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि मातृ भाषा में शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का मूलभूत अधिकार है। भारत एक बहुभाषी समाज है भाषायी विविधता हमारे देश की खूबसूरती है। वर्तमान केंद्र सरकार 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति 2020 में लेकर आई है जो एक सराहनीय कदम है। नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं और मातृ भाषाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, लेकिन नई शिक्षा नीति में मातृ भाषा और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराने की जो बात कही गई है उसका आधार क्या होगा? शिक्षा नीति में कोई स्पष्ट मानक तय नहीं किया गया है। क्या प्राथमिक शिक्षा आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में होगा या अन्य स्थानीय भाषाओं में जो आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है उनमें भी होगा, ये अनुत्तरित सवाल हैं। हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि हिंदी को अंग्रेजी की जगह राष्ट्र की सम्पर्क भाषा बना देना चाहिए, यह एक साहसिक बयान है। अमित शाह जी ने अपने बयान में बताया कि पूर्वोत्तर भारत की बोडो, जेमी, किरबुक सहित आठ स्थानीय भाषाओं द्वारा देवनागरी लिपि अपनाना कोई मामूली घटना नहीं है। वैसे भारतीय भाषाओं के देवनागरी लिपि अपनाने का विचार नया नहीं है। आचार्य विनोबा भावे ने भी कहा था कि भारतीय भाषाएं अगर देवनागरी लिपि अपना लें तो भारत की एकता अखंडता के लिए मजबूत प्रयास होगा। खासतौर पर दक्षिण की भाषाओं को इसका बड़ा लाभ होगा। वहां की चार भाषाएं अत्यंत निकट हैं, तेलूगु, मलयालम, कन्नड़ में बहुत सारे शब्द संस्कृत के हैं और इन भाषाओं में बहुत सारे शब्द समान हैं,अगर ये सभी नागरी लिपि स्वीकार कर लेते हैं तो दक्षिण के लोग चारों भाषाएं बहुत जल्द और आसानी से सीख सकते हैं। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि देश की सम्पर्क भाषा हिंदी बने। यह देश का दुर्भाग्य है जहां इतनी सारी भाषाएं हैं वहां एक विदेशी भाषा अंग्रेजी सम्पर्क भाषा बनी हुई है। अमित शाह जी के हिंदी के संबंध में दिए गए बयान के बाद दक्षिण भारत से कुछ नेताओं द्वारा हिंदी विरोध के स्वर मुखर फिर हुए जो वर्षो से दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन को हवा देते रहें हैं। हवा देने वालों में वामपंथी विचारधारा, सहित भारत की एकता अखंडता की विरोधी शक्तियों का महत्त्वपूर्ण एजेंडा है हिंदी विरोध। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। देश में 22 भाषाओं को आठवीं अनुसूची में मान्यता मिली हुई है मगर रिजर्व बैंक के नोट पर सिर्फ 15भाषाओं का प्रयोग होता है किसी ने विरोध नहीं किया। सेंट्रल यूनिर्वसटिी के अंदर स्नातक कोर्स के दाखिले के लिए 13 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं, जिस बात पर कोई विवाद या विरोध नहीं है। साहित्य अकादमी में 24 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी से मिलने वाले पुरस्कारों, लाभों से वंचित होना पड़ता है, ये भी विसंगति है। 2005 में कुछ दक्षिण भारतीय भाषाओं को जो 1500 साल से ज्यादा पुरानी थी, शास्त्रीय भाषा की मान्यता मिली किसी ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि एक मानक तय किया गया, जिसके आधार पर इन शास्त्रीय भाषाओं को उनका लाभ मिल रहा है, कोई विरोध नहीं है। परंतु आज तक आठवीं अनुसूची का कोई पैरामीटर नहीं बन पाया कि आखिर आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने का क्या मानक हो, 14-15 लाख की संख्या में बोलने वाली भाषाएं आठवीं अनुसूची में शामिल हैं, मगर 20 करोड़ की संख्या में बोली जाने वाली भोजपुरी जैसी कई भाषाएं आठवीं अनुसूची से अभी भी दूर हैं।
वर्तमान केंद्र सरकार का रवैया स्थानीय भाषाओं के प्रति कुछ सकारात्मक जरूर रहा है। यूपी में भोजपुरी, अवधी, बुंदेली और ब्रज भाषाओं की अकादमी बनने की आहट है। 34 वर्षो बाद केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लाकर अपनी रचनात्मकता को व्यक्त किया है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं और स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने की बात हो रही है ये अच्छी बात है, मगर आजादी के अमृत महोत्सव के बाद भी भारत राष्ट्र की अपनी कोई स्पष्ट भाषा नीति नहीं है, जिसके कारण कुछ नकारात्मक तत्व समय-समय पर हिंदी बनाम दक्षिण भारतीय भाषा, हिंदी बनाम भोजपुरी, हिंदी बनाम मराठी, हिंदी बनाम अंग्रेजी और हिंदी बनाम बंगाली विवाद को हवा देते रहते हैं। भाषायी नीतियों की अस्पष्टता के कारण बहुत सारी भाषाओं को उनके उचित हक से वंचित रहना पड़ता है जो यदा-कदा विवादों का कारण बनते हैं। जरूरत है कि जल्द-से-जल्द केंद्र सरकार भाषायी विवादों को दूर करने और विसंगतियों को खत्म कर आने वाली पीढ़ियों के भाषायी सौहार्द का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय भाषा नीति लेकर आए, तभी देश में अनुत्तरित भाषायी सवालों का हल निकल पाएगा और राष्ट्र के विकास की गति को तेज किया जा सकता है।
युद्ध के समय तेजी से भारत के करीब आता पश्चिम
हर्ष वी पंत, ( प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन )
जैसे-जैसे यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध बढ़ता जा रहा है, पश्चिम के साथ भारत के जुड़ाव में भी तेजी आ रही है। दिलचस्प है कि कई लोगों को आशंका थी कि यूके्रन-रूस युद्ध के समय में भारत पर पश्चिमी रुख के मुताबिक चलने के लिए दबाव डाला जाएगा, लेकिन अब रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्ते की वजहों को समझा जा रहा है। नई दिल्ली पहुंचने वाले यूरोपीय नेताओं का तांता लगा हुआ है। यूरोप और भारत के बीच संबंध लगातार बढ़ रहे हैं, दोनों पक्षों के नेतृत्व ने कई मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी गत दिनों भारत में थीं, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता के नुकसान, ऊर्जा और डिजिटल प्रसार, परस्पर संपर्क, सुरक्षा, रक्षा और हिंद-प्रशांत में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के रूप में उनकी यह पहली भारत यात्रा थी, जिसके दौरान उन्होंने भारत में एक कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित भी किया।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी पिछले सप्ताह भारत में थे और उनका दृष्टिकोण है कि भारत और ब्रिटेन के बीच पूरकता पर जोर देना है और रूस के मामले में परस्पर मतभेदों को कम करना है। जॉनसन ने भारत-रूस संबंधों के बारे में कहा कि यह एक ऐतिहासिक संबंध है, जिसे हर कोई समझता है और सम्मान करता है। इससे शायद कई ऐसे लोगों को आश्चर्य हुआ होगा, जिन्होंने उम्मीद की थी कि इस यात्रा के दौरान रूस पर एक विवादास्पद बहस सामने आएगी। पश्चिम में अनेक लोगों को भारत से शिकायत रही है कि वह यूक्रेन के मामले में पश्चिमी देशों के साथ नहीं है और अपनी अलग स्थिति बनाकर चलना चाहता है। वैसे भारत अपनी स्थिति को लेकर कतई रक्षात्मक नहीं है।
नई दिल्ली रूस के सवाल पर पूरी साफगोई से अपनी बात रख रही है। भारत में अनेक पश्चिमी नेताओं की मेजबानी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत-यूरोप साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए मई की शुरुआत में तीन यूरोपीय देशों, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। विदेश मंत्री, एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2+2 वार्ता के लिए पहले ही अमेरिका जा चुके हैं, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इतिहास में या आज गलत जगह खड़ा है, ऐसी धारणा से अमेरिका पीछे हट रहा है।
भारत किसी तरह की अनावश्यक बहस में नहीं उलझ रहा है, पूरी सफाई के साथ अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए चल रहा है। यदि पश्चिम को भारत को अपनी रणनीति में शामिल करना है, तो उसे भारत की दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करने में भागीदार बनना होगा, चाहे वह रक्षा हो या ऊर्जा। यही संदेश भारत अपने पश्चिमी समकक्षों को लगातार दे रहा है। भारतीय विदेश मंत्री तांत्रिक जवाबों के साथ पेश आ रहे हैं। भारत में एक नया विश्वास पाया गया है कि नई दिल्ली के विकल्प केवल अपनी सामरिक अनिवार्यताओं से संचालित होंगे।
पिछले कुछ वर्षों में भारतीय विदेश नीति के सामने सबसे महत्वपूर्ण मकसदों में से एक है, पश्चिम के साथ दीर्घकालिक स्थायी संबंध बनाना। इस लक्ष्य का पीछा करने में नई दिल्ली ने कुछ गंभीर कूटनीतिक पूंजी खर्च की है और नतीजे साफ हैं। बेशक, पश्चिम को भी भारत की बदलती उम्मीदों और हिंद-प्रशांत में उभरती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ आना पड़ा है। लंबे समय से यूरोपीय संघ ऐसे किसी प्रयास से बच रहा था, लेकिन जैसे-जैसे चीन की ओर से दबाव बढ़ा और रूस ने यूरोप की सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा कर दी, यूरोप को बदलाव के लिए तैयार होना पड़ा। खासकर पश्चिम यूरोपीय देश नई विदेश नीति विकसित करने को मजबूर हो रहे हैं। अब यूरोप समान विचारधारा के देशों के साथ भागीदारी बढ़ाना चाहता है।
इस नए समीकरण में भारत-यूरोपीय संघ की साझेदारी निश्चित रूप से यूरोपीय संघ के लिए महत्वपूर्ण है, यह देखते हुए कि यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और एक खास रणनीतिक महत्व वाला देश बना हुआ है।
आज जब भारत की बात आती है, तो यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पद्र्धा भी दिखाई पड़ती है। दोनों भारत के साथ लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि रूस-यूक्रेन युद्ध से संकट, पश्चिम के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को मजबूत करेगा और यह भारतीय कूटनीति की असली कामयाबी है।
