
25-07-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:25-07-20
Date:25-07-20
Sisters in arms
Army women win a battle for equal opportunities
TOI Editorials
Five months after the Supreme Court verdict that the army’s short service commission women are entitled to permanent commission, no matter how long they have served, the Centre has acceded to the order. This case only covers women in ten streams like army air defence, signals, engineers, service and intelligence corps – but is still a win for equal work opportunities. This is one heartening step in the journey to gender parity in the military. So far, women make up only 3.89% of the Indian army, 6.7% in the navy and 13.2% in the air force, excluding the various medical services.
The more fraught question of women in direct combat roles still remains to be addressed. While women will have to pass exacting standards to prove themselves fit for these roles, as do men, there is no place for worries about unit cohesion, or patriarchal ideas of honour and protection. The physical and mental standards for the role must be uniform and gender-neutral, and women and men free to compete for them.
Mindsets have changed, young men today are more used to seeing women as peers, and occupying leading public roles. A woman commanding them in combat would not blow their mind, as it might have older generations of army men. Women will need separate barracks and toilets, and there must be clear anti-harassment policies. The average male default in military equipment must now also accommodate other bodies.
Politics of last resort
In India the compact between voter and legislator is all too easily broken
Sadanand Dhume
If an alien landed on Earth and demanded to see an Indian legislator in his natural habitat, where would you send him? My pick: an upscale resort hotel. Among freshly mown lawns, long buffet tables, and flat screen TVs showing Bollywood reruns, the odds of sighting a state legislator would appear fairly high. (MPs tend to be more elusive.)
If schlepping it to a hotel in Manesar, or Mumbai, or the outskirts of Bangalore, seems like too much effort, you could just turn on the television instead and watch excitable anchors and political pundits analyse “the numbers game.” Will the rebel legislators herded into a resort succeed in toppling an elected government? Or will the wily chief minister, holed up with his flock in another hotel, keep the wolves at bay?
The venue for this month’s drama is Rajasthan. But from recent memory you could easily swap it for Karnataka, Maharashtra or Madhya Pradesh by changing just a few details – like the homesick MLA who asks a chef to make paranthas rather than poha. While the ending may vary from state to state, the drama’s setting (a resort or hotel) and characters (sitting legislators) remain unchanged.
In the Rajasthan crisis, newspapers speculate that the going price for a state legislator to switch parties ranges between Rs 15-25 crore, or $2.25 million to $3.75 million, a staggering sum in any country, but particularly so in one whose annual per capita income hovers around $2100. But what’s shocking is not the figures bandied about; it’s that people have lost the capacity to be shocked. In India, the idea of a legislator with a price tag has become as commonplace as the expectation that a fashion model be tall or a doctor wear a white coat.
No single party bears all the blame. With its bottomless pockets, these days the ruling Bharatiya Janata Party plays destabiliser-in-chief while Congress struggles to keep its state governments intact. In Maharashtra, last year, it was the Shiv Sena that hastily betrayed the voters’ mandate by abandoning a coalition with BJP that enjoyed popular legitimacy. Nor did Congress or the Nationalist Congress Party come out smelling like roses. Suffice to say that most elected politicians spring from a common culture.
Even the Aam Aadmi Party, birthed in an anti-corruption movement that captured the middle class imagination nine years ago, turned out not to be that different. Faced with electoral reality, the party’s promises of radical transparency and a new kind of politics quickly faded. In hindsight, Arvind Kejriwal’s shrill diatribes against the trappings of power like government bungalows and official cars suggested longing more than revulsion. Nobody should be surprised that the prominent do-gooders who helped give AAP its moral sheen at the outset did not last very long in the party.
Prime Minister Narendra Modi may have largely retained his clean image, but BJP no longer even pretends to be “the party with a difference.” Nor do its supporters seem to care particularly. Many of them have no qualms about the party leadership playing dirty, as long as it plays to win. They are like supporters of a long-suffering soccer team that has learned how to expertly foul opponents and suddenly starts lifting championship trophies. Winning is all that matters.
Campaign finance lies at the heart of the defection problem. Elections cost a lot of money and a ministerial position is widely seen as a means to recoup investment. Here BJP has the dubious distinction of touting a reform – electoral bonds – that has arguably made the problem worse. According to Carnegie Endowment for International Peace scholar Milan Vaishnav, “by their design, electoral bonds legitimise opacity in how elections are funded.”
What does a willingness to switch loyalties so easily say about the compact between voter and elected representative? In the late 18th century, Edmund Burke famously told his constituents in Bristol that they could not expect him to blindly follow their wishes in Parliament. According to Burke, as a Member of Parliament he only owed his constituents “the clearest conviction of his judgment and conscience.” He expected them to elect him for his discernment, not as a mere rubber stamp.
As populism has swept the West, this Burkean ideal has come under stress. According to a YouGov poll last year, four-fifths of British MPs agreed with Burke, but only 7% of voters shared his view of representation. In India, forget about “judgment and conscience.” You can’t even be sure that the person you voted for because they stood for one set of ideas won’t turn around and join a party that stands for the opposite.
What does all this mean for Indian democracy? If you’re an optimist, you can look at it as a phase. Few democracies have followed Singapore’s path of squeaky cleanliness from the start. Many countries with relatively ethical politics today did not look that different from India a hundred years ago.
If you’re a pessimist, however, you have to wonder if the breakdown of the most elementary trust between voter and legislator points toward something more troubling, a signpost along the road to the delegitimisation of democracy. Will the rotten plank that resort politics represents eventually bring down the entire house?
Case for presidential system
It has never been clearer. The disrepute into which the political process has fallen in India, and the cynicism about the motives of politicians, can be traced to the workings of the parliamentary system.
Shashi Tharoor, [Lok Sabha MP from the Congress.]
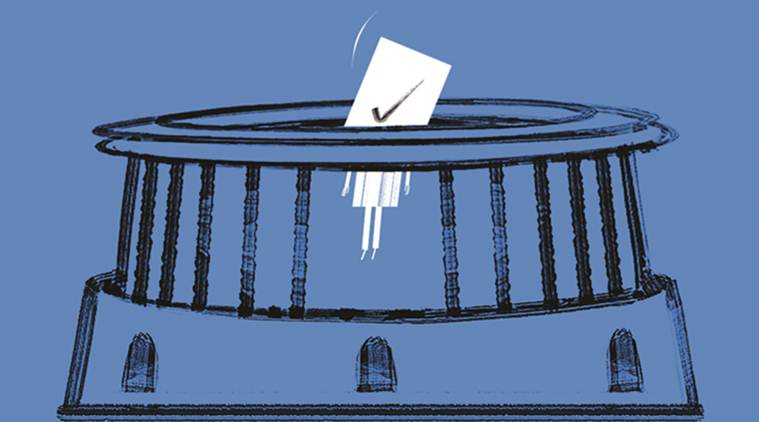
The disgraceful political shenanigans the nation has witnessed, most recently in Karnataka, Madhya Pradesh and Rajasthan, and the horse-trading of MLAs to switch allegiances for power and pelf, are not merely an occasion for breast-beating about morality in politics or the opportunism of the cash-rich ruling party. We never seem to look beyond the headlines to the basic problem: The system that makes this shameful conduct possible. The parliamentary system we borrowed from the British has not worked in Indian conditions. It is time to demand a change.
The facts are clear: Our parliamentary system has created a unique breed of legislator, largely unqualified to legislate, who has sought election only in order to wield executive power. It has produced governments dependent on a fickle legislative majority, who are therefore obliged to focus more on politics than on policy or performance. It has distorted the voting preferences of an electorate that knows which individuals it wants to vote for but not necessarily which parties. It has spawned parties that are shifting alliances of selfish individual interests, not vehicles of coherent sets of ideas. It has forced governments to concentrate less on governing than on staying in office, and obliged them to cater to the lowest common denominator of their coalitions. The parliamentary system has failed us.
Pluralist democracy is India’s greatest strength, but its current manner of operation is the source of our major weaknesses. To suggest this is political sacrilege in India. Barely any of the many politicians I have discussed this with are even willing to contemplate a change. The main reason for this is that they know how to work the present system and do not wish to alter the ways they are used to.
Yet the parliamentary system devised in Britain — a small island nation with electorates of less than a lakh voters per constituency — is based on traditions which simply do not exist in India. These involve clearly defined political parties, each with a coherent set of policies and preferences that distinguish it from the next, whereas in India a party is all-too-often a label of convenience which a politician adopts and discards as frequently as a Bollywood film star changes costume. Hopping from one to the next — which would send shock waves through the political system in other parliamentary democracies — is commonplace, even banal, in our country.
In the absence of a real party system, the voter chooses not between parties but between individuals, usually on the basis of their caste, their public image or other personal qualities. But since the individual is elected in order to be part of a majority that will form the government, party affiliations matter. So voters are told that if they want a Narendra Modi as prime minister, or a Mamata Banerjee or Jagan Reddy as their chief minister, they must vote for someone else as MP or MLA in order to indirectly accomplish that result. It is a perversity only the British could have devised — to vote for a legislature not to legislate but in order to form the executive.
The fact that the principal reason for entering Parliament is to attain governmental office creates four specific problems. First, it limits executive posts to those who are electable rather than to those who are able. The prime minister cannot appoint a cabinet of his choice; he has to cater to the wishes of the political leaders of several parties. (Yes, he can bring some members in through the Rajya Sabha, but our upper house too has been largely the preserve of full-time politicians, so the talent pool has not been significantly widened.
Second, it puts a premium on defections and horse-trading. The anti-defection Act of 1985 has failed to cure the problem, since the bargaining has shifted to getting enough MLAs to resign to topple a government, while promising them offices when they win the subsequent by-elections.
Third, legislation suffers. Most laws are drafted by the executive — in practice by the bureaucracy — and parliamentary input into their formulation and passage is minimal, with very many bills being passed after barely a few minutes of debate. The ruling party inevitably issues a whip to its members in order to ensure unimpeded passage of a bill, and since defiance of a whip itself attracts disqualification, MPs blindly vote as their party directs. The parliamentary system does not permit the existence of a legislature distinct from the executive, applying its collective mind freely to the nation’s laws. Accountability of the government to the people, through their elected representatives, is weakened.
Fourth, for those parties who do not get into government and who realise that the outcome of most votes is a foregone conclusion, Parliament or Assembly serves not as a solemn deliberative body, but as a theatre for the demonstration of their power to disrupt. The well of the house — supposed to be sacrosanct — becomes a stage for the members of the opposition to crowd and jostle, waving placards and chanting slogans until the Speaker, after several futile attempts to restore order, adjourns in despair. In India’s Parliament, many opposition members feel that the best way to show the strength of their feelings is to disrupt law-making rather than debate the law.
Apologists for the present system say in its defence that it has served to keep the country together and given every Indian a stake in the nation’s political destiny. But that is what democracy has done, not the parliamentary system. What our present system has not done as well as other democratic systems might, is to ensure effective performance. India’s many challenges require political arrangements that permit decisive action, whereas ours increasingly promotes drift and indecision. We must have a system of democracy whose leaders can focus on governance rather than on staying in power.
The disrepute into which the political process has fallen in India, and the widespread cynicism about the motives of our politicians, can be traced directly to the workings of the parliamentary system. Holding the executive hostage to the agendas of a motley bunch of legislators is nothing but a recipe for governmental instability. And instability is precisely what India, with its critical economic and social challenges, cannot afford.
The case for a presidential system has, in my view, never been clearer. A directly elected chief executive in New Delhi and in each state, instead of being vulnerable to the shifting sands of coalition support politics, would have stability of tenure free from legislative whim, be able to appoint a cabinet of talents, and above all, be able to devote his or her energies to governance, and not just to government. The Indian voter will be able to vote directly for the individual he or she wants to be ruled by, and the president will truly be able to claim to speak for a majority of Indians rather than a majority of MPs. At the end of a fixed period of time, the public would be able to judge the individual on performance in improving the lives of Indians, rather than on political skill at keeping a government in office.
The same logic would apply to the directly elected heads of our towns and cities — as I have proposed in a Private Member’s Bill in the Lok Sabha — and village panchayats, who today are little more than glorified committee chairmen, with little power and minimal resources. To give effect to meaningful local self-government, we need directly elected local officials, each with real authority and financial resources to deliver results in their own areas.
The only serious objection advanced by liberal democrats is that the presidential system carries with it the risk of dictatorship. They conjure up the image of an imperious president, immune to parliamentary defeat and impervious to public opinion, ruling the country by fiat. In particular they argue that it will pave the way for a Modi dictatorship in India. But a President Modi could scarcely be more autocratic than the prime minister we have seen in office — one who has, thanks to the parliamentary system, a rubber-stamp majority in the Lok Sabha rather than the independent legislature a presidential system would ensure. In addition, the powers of a President Modi would be amply balanced by those of the directly elected chief executives in the states, who would be immune to dismissal by their party leader, or to toppling by defecting MLAs.
Democracy is an end in itself, and we are right to be proud of it. But few Indians are proud of the kind of politics our democracy has inflicted upon us. With the needs and challenges of one-sixth of humanity before our leaders, we must have a democracy that delivers progress to our people. Changing to a presidential system is the best way of ensuring a democracy that works.
Date:25-07-20
Judicial indiscipline
Rajasthan HC has disregarded law laid down by SC while admitting plea by Pilot camp
Editorial
The Rajasthan High Court’s order, directing that status quo be maintained in the disqualification proceedings against 19 legislators and holding a legal challenge to the Rajasthan Assembly Speaker’s notice under the anti-defection law to be maintainable, borders on judicial indiscipline. The order does not give any reason for admitting the petition and overruling objections to its admissibility, except for saying legal questions have arisen, including one on the validity of a sub-clause in the Tenth Schedule. It is as if the mere fact that some questions have arisen is enough to disregard the doctrine of precedent. There is a specific prohibition in a Constitution Bench verdict of the Supreme Court on courts intervening in disqualification matters at a stage prior to a presiding officer giving a ruling. Of the 13 questions the Division Bench has framed, purporting to arise from the Speaker C.P. Joshi’s notices to 19 Congress members in the Sachin Pilot camp, the last one itself shows it cannot entertain the petition. The question is whether the Supreme Court’s judgment in Kihoto Hollohan (1992) is a bar on the High Court examining the issues. It is illogical that the Bench holds that the petition is maintainable even while proposing to examine whether a Constitution Bench judgment binds it or not. In other words, a petition has been declared maintainable on the ground that the court proposes to examine its maintainability. And the 1992 judgment, while upholding the validity of the Tenth Schedule to the Constitution, the anti-defection law, also declared that Para 2 — a part of which is now under challenge and is the ostensible reason for the High Court to entertain the petition — does not violate the freedom of speech, vote or conscience of elected members. Yet, the High Court is now venturing to find out whether Para 2(1)(a), which deals with disqualifying lawmakers who “voluntarily give up membership” of their party, has been examined by the apex court from the point of view of “intra-party democracy”. If at all the provision’s validity is to be tested, it can only be done in a case arising out of it. When no decision has been rendered by the Speaker, it is beyond comprehension how the court entertained arguments on the issuance of the notice and on whether dissidents can be disqualified for questioning the party line. Para 2(1)(a) has been used by Speakers for years, and many such disqualification orders have been upheld by the Supreme Court, including as recently as November 2019 in a Karnataka case. Admitting a matter without explaining how the law laid down by the Supreme Court does not bind a High Court raises grave questions of judicial propriety. However, even as the political crisis plays out on the lawns of Raj Bhavan, the top court itself appears to be raising the question whether dissent within a party can attract disqualification proceedings. Whatever the circumstances, the SC should not condone improper and premature judicial intervention.
कृषि सुधारों से परिचित हों किसान
पुष्पेंद्र सिंह, (लेखक किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं)

बीते दिनों केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु लाए गए अपने दो अध्यादेशों को अधिसूचित कर दिया, परंतु उनके प्रति किसानों के मन में कुछ शंकाएं दिख रही हैं। 20 जुलाई को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ किसान संगठन इनके विरोध में सड़कों पर भी उतरे। दरअसल किसानों को यह शंका है कि इन सुधारों के बहाने सरकार एमएसपी व्यवस्था समाप्त करने की ओर बढ़ रही है। सच्चाई यह है कि ये सुधार कृषि उपज की बिक्री हेतु पहले की व्यवस्था के साथ-साथ एक अन्य समानांतर व्यवस्था बना रहे हैं। यह किसानों के विवेक और पसंद पर निर्भर होगा कि वे किस व्यवस्था के अंतर्गत अपनी फसल बेचना चाहते हैं।
किसानों को यह भी समझना होगा कि नई व्यवस्था एक नया विकल्प है, जो वर्तमान मंडी व्यवस्था के साथ-साथ चलता रहेगा। हमारा कृषि क्षेत्र लगभग आधी आबादी को रोजगार देता है। देश की कृषि जीडीपी लगभग 30 लाख करोड़ रुपये की है, पर देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी मात्र 15 प्रतिशत है। साफ है कि कृषि क्षेत्र में सुधारों का असर आधी आबादी की आय पर पड़ेगा।
एक अध्यादेश के जरिये कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में सुधार करते हुए किसानों को अधिसूचित मंडियों के अलावा भी अपनी उपज को कहीं भी बेचने की छूट प्रदान की गई है। इससे किसान अपनी उपज को जहां उसे उचित और लाभकारी मूल्य मिले वहां बेच सकते हैं। इस विषय में चार बड़े सुधार किए गए हैं। पहला, अब तक कृषि उत्पादों को केवल स्थानीय अधिसूचित मंडी के माध्यम से ही बेचने की अनुमति थी। अब किसी भी मंडी, बाजार, संग्रह केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, कारखाने आदि में फसलों को बेचने के लिए किसान स्वतंत्र हैं। इससे किसानों का स्थानीय मंडियों में होने वाला शोषण कम होगा और फसलों की अच्छी कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी। अब किसानों के लिए पूरा देश एक बाजार होगा।
तीसरा, मंडी के बाहर फसलों का व्यापार वैध होने के कारण मंडी व्यवस्था के बाहर भी फसलों के व्यापार और भंडारण संबंधित आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ेगा। चौथा, अब अन्य राज्यों में उपज की मांग, आर्पूित और कीमतों का र्आिथक लाभ किसान स्वयं या किसान उत्पादक संगठन बनाकर उठा सकते हैं। किसानों को स्थानीय स्तर पर अपने खेत या घर से ही सीधे किसी भी व्यापारी को फसल बेचने का अधिकार होगा। इससे किसान का मंडी तक फसल ढोने का भाड़ा भी बचेगा।
अभी तक मंडी में पहुंचने के बाद सही मूल्य न मिलने पर भी किसान फसल बेचने को मजबूर होता था, क्योंकि वापसी का भाड़ा देना और नुकसानदायक होता। यदि फसल जल्द खराब होने वाली उपज हो तो मंडी पहुंचने के बाद उसे किसी भी मूल्य पर बेचने की मजबूरी होती है। किसान की इसी मजबूरी का लाभ बेचौलिये उठाते रहे हैं। अब किसान अपने घर या खेत से उचित मूल्य मिलने पर ही फसल बेचेगा। किसानों को मंडियों की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, लंबी कतारों, लंबे इंतजार से भी मुक्ति मिलेगी। प्रतिस्पर्धा के कारण इन मंडियों को भी अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
दूसरा अध्यादेश अनुबंध कृषि से संबंधित है जो फसल की बुआई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे किसान एक तो फसल तैयार होने पर सही मूल्य न मिलने के जोखिम से बच जाएंगे, दूसरे उन्हें खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं होगा। किसान सीधे थोक और खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों, प्रसंस्करण उद्योगों आदि के साथ उनकी आवश्यकताओं और गुणवत्ता के अनुसार फसल उगाने के अनुबंध कर सकते हैं। इससे किसानों को फसल उगाने से पहले ही सुनिश्चित दामों पर फसल का खरीददार तैयार मिलेगा। इसमें किसानों की जमीन के मालिकाना अधिकार सुरक्षित रहेंगे और उसकी मर्जी के खिलाफ फसल उगाने की कोई बाध्यता भी नहीं होगी। इसमें फसल खराब होने के जोखिम से भी किसान का बचाव होगा।
किसान खरीददार के जोखिम पर अधिक जोखिम वाली फसलों की खेती भी कर सकता है। कृषि जिंसों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी सुगम बनाया जा रहा है। इसी तरह कृषि उत्पादों को ई-ट्रेडिंग के माध्यम से बेचने की सुविधा को बेहतर बनाया जा रहा है। किसानों को अपनी उपज के लाभकारी मूल्य प्राप्ति हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किए गए हैं। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज सहित सभी कृषि खाद्य पदार्थ अब नियंत्रण से मुक्त होंगे। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी।
चूंकि एमएसपी व्यवस्था केवल गेंहू, धान जैसी कुछ फसलों और कुछ राज्यों तक ही वास्तविक रूप से सीमित रही है अत: एमएसपी की वर्तमान व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। किसानों से एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद र्विजत हो और इसके उल्लघंन पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाए। दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स के प्रावधानों में भी एकरूपता होनी चाहिए। दोनों व्यवस्थाओं का समानांतर चलना किसान हित में आवश्यक है।
पाताल को जाता भूजल
संपादकीय
गोरखपुर : सावधान, पाताल का जल नीचे खिसक रहा है। दो साल पहले तक सरकारी महकमा पूर्वाचल में भूगर्भ जल स्तर सुरक्षित जोन होने का दावा करता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। जल के लगातार हो रहे दोहन से घटते जल स्तर ने चिंता बढ़ा दी है, बावजूद इसके संकट से निपटने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। उल्टे शासन-प्रशासन की उदासीनता के कारण कहीं ताल- पोखरों का अतिक्रमण कर जल प्रबंधन के परंपरागत स्रोतों को बंद किया जा रहा है तो शहरी हिस्से में आधुनिक तकनीक से बनने वाली बहुमंजिली इमारतों को मजबूत आधार देने के लिए धरती की कोख को बेपानी किया जा रहा है। जल के भरोसे जीवन जीने वाले आम नागरिक भी इसे लेकर बेपरवाह हैं। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भूगर्भ जल संरक्षण के लिए अत्यंत जरूरी माने जाने वाले वर्षा जल संचयन अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपायों पर न तो निजी आवासों और न ही सरकारी कार्यालयों में अमल हो रहा है। सर्वे रिपोर्ट बताती है कि भारत में पृथ्वी का जलस्तर औसतन तीन से चार फीट प्रतिवर्ष गिर रहा है और इसका प्रभाव पूर्वाचल पर भी पड़ना स्वभाविक है, फिर भी सरकारी महकमा आंख मूंदे हुए है। भूगर्भ जल के दोहन का पैमाना माने जाने वाले विकास दर की रिपोर्ट भी चौंकाने के लिए पर्याप्त है।
वर्षा का जल प्रकृति का अनमोल उपहार है। जल प्रबंधन की जागरुकता के अभाव में यह जल काफी हद तक बेकार हो जाता है। लोग यह नहीं समझने की कोशिश करते कि इस जल का प्रबंध कर दिनचर्या के तमाम कार्य निपटाए जा सकते हैं। साथ ही इससे भूमिगत जल रिचार्ज भी हो सकता है।
भूगर्भ जल विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक चरगांवा, भटहट, पिपराइच एवं बड़हलगंज ब्लाक में भूगर्भ जल स्तर पांच मीटर है। बाकी ब्लाकों में .09 मीटर से 1.96 मीटर के बीच नीचे आया है। यह खतरे का संकेत है।
भूगर्भ जल का स्तर बरकरार रखने के लिए जितना दोहन (डिस्चार्ज) हो, उसी अनुपात में संचयन (रिचार्ज) जरूरी है। संचयन की कई प्रणालियां प्रयोग में लायी जा सकती हैं। इसमें परंपरागत जल स्रोत के रूप में ताल-पोखरे, कुंए, झीलें, नदियां हैं। आधुनिक तरीकों में रूफ टाप (मकान की छतों से) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली सर्वाधिक प्रचलित है। पक्के मकानों की छत पर वर्षा जल को एकत्र कर पाइप के माध्यम से जमीन पर लाया जाता है और वहां उसे एक टंकी में एकत्र किया जाता है। इस प्रकार संचित जल का समुचित शोधन कर प्रयोग में लाया जा सकता है जिससे न केवल भूजल पर निर्भरता में कमी आती है बल्कि ऐसे अनेक स्थानों पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इसी प्रकार किसी भी आवासीय परिसर में वर्षा जल को एकत्र कर नालियों के माध्यम से किसी स्थान पर लाया जाता है और वहां पर भूमिगत पाइप के माध्यम से उसे भूजल के रिचार्ज के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।
भूजल के रिचार्ज की दर दोहन की मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। गोरखपुर व बस्ती मंडल में महराजगंज व कुशीनगर को छोड़कर अन्य जिलों में भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है अत: दोनों मंडलों में भूजल के अंधाधुंध प्रयोग पर नियंत्रण की आवश्यकता है बल्कि वर्षा जल संचयन एवं हरित आच्छादन व वनाच्छादन को बढ़ावा देकर भूजल को सामान्य स्थिति में लाने में मदद मिलेगी। इससे भूजल की गुणवत्ता में भी धीरे-धीरे सुधार आएगा
भूगर्भ जल बारिश, नदियों व पोखरों के जरिए संचित होता है। दोहन के हिसाब से संचयन हो तो समस्या नहीं हो सकती है। गोरखपुर क्षेत्र में इसमें असंतुलन पैदा हुआ है जो निश्चित ही खतरे का संकेत है। इसके लिए सबसे पहले ताल-पोखरों पर अतिक्रमण रोकना होगा।
सिर्फ अपने हित की राह चले देश
जोरावर दौलत सिंह, (फेलो, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज)
अर्थव्यवस्था में चीन की भावी भूमिका को लेकर भारत में बहस गरम है। मगर इससे जुड़े कुछ बुनियादी सवाल हैं, जिन्हें नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे, चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध का ही मामला लें। इसका मुख्य मकसद यह संकेत देना था कि सीमा पर बनाए गए दबाव की यह कीमत है। और विवेकपूर्ण ढंग से यदि इसे अमल में लाया गया, तो इससे बीजिंग का रुख प्रभावित होगा। मगर, आर्थिक कार्ड की ब्रांडिंग इस तरह नहीं की जा सकती, और स्थानीय आजीविका, भारत के अपने आधुनिकीकरण के प्रयासों और भू-राजनीतिक लक्ष्यों पर इसके पड़ने वाले असर के बारे में हमारे नीति-निर्माताओं को सजग रहना चाहिए।
दिल्ली को वैश्विक अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक रुझानों के बारे में भी चिंतन करना चाहिए, खासतौर से अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी की प्रकृति को देखकर, और आने वाले वर्षों में वैश्वीकरण की दशा-दिशा का अनुमान लगाकर। सवाल कई हैं। जैसे, आगामी वर्षों में अमेरिका और चीन किस हद तक आपसी तनाव बढ़ाएंगे? क्या हमें भू-आर्थिक प्रतिस्पद्र्धा के इस युग में एक तरफ झुक जाना चाहिए? क्या भारत के लिए यह एक मौका है कि वह बाजार में विविधता की इच्छा रखने वालों और वैश्विक उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दे?
यदि हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि भारत को उच्च प्रौद्योगिकी वाले औद्योगिकीकरण, अधिक गुणवत्ता वाले विनिर्माण-कार्य, उत्पादों की आपूर्ति से जुड़ी व्यवस्था में अधिकाधिक रोजगार, और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की दरकार है, तो वैश्वीकरण में खलल डालने वाले इन रुझानों का समझदारी से लाभ उठाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त हमारा एक रणनीतिक लक्ष्य अपने पारंपरिक रिश्ते को फिर से जिंदा करना भी है, यानी इंडो-पैसिफिक और यूरेशियाई पड़ोसी देशों के साथ अपने कारोबारी व सामाजिक संपर्क बढ़ाना। इस परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में चीन की भूमिका को आखिर किस तरह गढ़ा जाना चाहिए? पिछले छह वर्षों से मोदी सरकार का रुख यही रहा है कि व्यापार घाटे को नियंत्रित किया जाए और देश में चीनी निवेश व प्रौद्योगिकी को आकर्षित किया जाए। इसके लिए द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को व्यापक और संतुलित बनाने की कोशिशें हो रही हैं, ताकि आपसी कारोबार में वह हावी न रहे, और रिश्ता निवेश-उन्मुख बने। आज औद्योगिक उपकरण, कल-पुर्जे, तकनीक, प्रौद्योगिकी आदि को लेकर चीन पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक है, जिससे यह बखूबी समझा जा सकता है कि नई दिल्ली और बीजिंग किस तरह एक-दूसरे पर निर्भर हैं।
इसीलिए, बिना सोचे-समझे चीन से अलग होने की राह हमें नहीं अपनानी चाहिए। इसकी बजाय, तमाम क्षेत्रों में और अर्थव्यवस्था के लिए हमें ऐसा अध्ययन करना चाहिए कि किस तरह हम लागत से अधिक फायदा कमा सकते हैं, और इसका क्या असर पड़ेगा। ऐसे आकलनों के बाद ही नीति-नियंताओं को चुनिंदा क्षेत्रों में चीन के साथ परस्पर-निर्भरता विकसित करने की नीति बनानी चाहिए या किसी अन्य देश से आयात बढ़ाकर और दूसरी जगहों से आउटसोर्सिंग करके इसे कम करने की योजना पर काम करना चाहिए। हमें सबसे पहले चीन की 2025 योजना की तरह प्रभावी औद्योगिकीकरण की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, और फिर पता करना चाहिए कि जिस तरह से चीन की सुधार प्रक्रिया में अमेरिका उत्प्रेरक बना था, उस तरह वह हमारे कैसे काम आ सकता है?
विशेषकर डिजिटल क्षेत्रों में अमेरिका और चीन में जो मुकाबला चल रहा है, उससे एक अन्य नीतिगत चुनौती हमारे सामने है। एक डिजिटल सुपरपावर को छोड़कर दूसरे के पाले में जाने से हमें बचना होगा। आखिरकार, चीनी और अमेरिकी कंपनियां समान धरातल पर हैं। दोनों से समान रूप से हमारी डाटा संप्रभुता को खतरा है। आयातित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए भी हमारी इन दोनों देशों पर निर्भरता है और दोनों ही हमारी स्थानीय क्षमताओं पर समान रूप से चोट करते हैं। लिहाजा, अपना बहुमूल्य संसाधन उन्हें सौंपने से पहले, हमें घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए।
एक अन्य विषय इंडो-पैसिफिक के साथ भारत का रिश्ता है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरईसीपी) पर हुआ फैसला बताता है कि भारत व्यापार के दरवाजे बंद करने को लेकर जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था अभी कमजोर है और कई तरह की संरचनात्मक समस्याएं हैं। स्थानीय स्तर पर भारत बेशक चीजों को व्यवस्थित करना शुरू करे, पर अमेरिका-चीन के बिगड़ते रिश्ते के बरअक्स हमारी क्षेत्रीय भू-आर्थिकी नहीं तैयार होनी चाहिए। सच यही है कि चीन और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों में गिरावट चीन-एशिया की परस्पर निर्भरता को कम नहीं करेगी। इसकी झलक हाल के आंकड़ों में दिखती है। पिछले साल आसियान उसके साथ द्विपक्षीय कारोबार करने वाला दूसरा बड़ा सहयोगी बन गया है। यह स्थान पहले अमेरिका का था। इस साल तो अब तक आसियान यूरोपीय संघ को भी पीछे छोड़ चीन से सबसे ज्यादा कारोबार करने लगा है।
ऐसे में, यदि अमेरिका एशिया को लेकर व्यावहारिक आर्थिक रणनीति नहीं बनाता, तो अंदाजा यही है कि चीन के अपने क्षेत्रीय और समुद्री पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंध कहीं ज्यादा गहरे होंगे। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अगला अमेरिकी राष्ट्रपति चीन को वार्ता की मेज पर लाने के लिए एशिया के प्रति क्या रुख अपनाएगा, लेकिन भारत अपनी कुशलता से उन दोनों की इस प्रतिस्पद्र्धा से फायदा उठा सकता है।
साफ है, अमेरिकी सियासत की संभावनाओं पर चिंतन करने की बजाय हमें भू-आर्थिकी और क्षेत्र में विकसित होने वाले रिश्तों को लेकर रणनीति बनानी चाहिए, ताकि हमारे लिए आगे के अवसर पैदा हो सकें। बेशक चीन के साथ संबंध प्रतिस्पद्र्धी और जटिल रहने के कयास हैं, लेकिन यदि हमें एशियाई देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है, तो पड़ोस में भू-आर्थिक रणनीतियों को तैयार करने की क्षमता हमें हासिल करनी ही होगी। भारत के पड़ोसी देश सहित कई एशियाई देश अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप की प्रौद्योगिकी व पूंजी का लाभ उठाने के लिए उदार रणनीति अपनाएंगे। ऐसे में, कुछ अलग करने की कोशिश करके हम प्रतिस्पद्र्धी लाभ और भविष्य की अपनी हैसियत को कम करने का जोखिम ही मोल लेंगे।
