
24-06-2024 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date: 24-06-24
Date: 24-06-24
Fix It, GOI
The future of India’s young depends on govt thinking creatively on reforming exams
TOI Editorials
Misery piles on for our young examinees. Last Wednesday, education ministry cancelled UGC-NET exam, conducted a day earlier, fearing a paper leak. On Saturday, it postponed NEET-PG exam scheduled for the next day, over “logistical issues”. When seen together with NEET-UG controversies, the message is loud and clear: something is seriously wrong with the National Testing Agency’s (NTA) functioning. And fixing the problem poses the first big challenge for new NDA govt.
Problems evident for long | The crisis may have blown up this year, but the signs have been there for years. Exams like NEET and JEE conducted by NTA have run into controversies regularly. In NEET 2022, CBI had to step in following allegations of impersonation in the exam. In 2021, a Russian hacker even hacked into the software for that year’s JEE to help examinees cheat.
It is the reluctance of authorities to take timely action against such episodes that is responsible for the present mess. This was made clear, when despite ample evidence, the education ministry remained in denial of a paper leak in this year’s NEET, ordering a CBI inquiry only on Saturday.
Remedy has failed us | What is galling is that NTA was put in place precisely to weed out issues we are facing today. So, one of the questions that needs to be asked is whether there are in-built flaws in conducting a mammoth exam like NEET, with 2.4mn examinees taking it in 13 languages across 4,500 centres.
It is welcome that govt has set up a high-powered committee to examine NTA’s functioning and recommend ways for fair conduct of exams. It has also brought into effect the Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 to prevent use of unfair means in public exams.
Nothing should be off table | But the panel’s work will have to be more than a bureaucratic exercise if the system is to be rid of its flaws. We need genuine reforms that address the spectrum of concerns that experts have been raising. The use of technology that allows algorithmic question patterns is one answer to paper leaks in avast system with innumerable nodes. Conducting exams more than once a year, as is the case in US, is another option to be considered. But decentralising the exams altogether is an option govt mustn’t shy away from. The future of young Indians is at stake.
Mend, Don’t Throw Away the Safety NTA
ET Editorials
The haste to damn the National Testing Agency (NTA) and the politicisation of what isn’t the agency’s finest moments is unfortunate. GoI’s move to address the problem of leaks and irregularities by setting up a time-bound committee headed by former Isro head and chair of IIT Kanpur board of governors, K Radhakrishnan, is the right first step. A common test for all applicants is a good idea. It reduces complexity, costs and ensures level playing field for applicants. Institutions are assured of a floor of the intakes’ aptitude.
Fixing NTA will also require regaining public trust. The committee must engage with stakeholders as well as experts, who can provide guidance on creating fail safes to localise and minimise impacts should the system be breached. Options for leveraging technology to improve the process and system — drawing on successful practices of similar organisations like ETS in the US — should be on the agenda.
GoI must be transparent and inclusive in its repair job. The committee’s report and work products should be made available on relevant websites including those of NTA and education ministry. GoI’s response to the recommendations and plan of action should be available for a time-bound public consultation finalisation. A time-bound implementation with regular audits would help restore trust.
The biggest vulnerability is the demand-supply gap. Nearly 24 lakh aspirants took the 2024 undergraduate medical test, NEET, for admission to 91,000 seats. As long as the ratio of aspirants to seats remains this high, there will be consistent and innovative efforts — some legal like coaching centres, and illegal to game the system. As the committee begins its work, the ministry should start working on addressing this mismatch.
Limit and excess
Creamy layer should be kept out, but the ceiling on quota is artificial
Editorial
The Patna High Court judgment striking down enhanced reservation for various communities in employment and education marks yet another instance of the strict application of the 50% ceiling on total reservations by the judiciary. The verdict has invalidated the Nitish Kumar regime’s decision of last year to amend its quota law to raise Backward Classes (BC) reservation from 12% to 18%, that of Extremely Backward Communities (EBC) from 18% to 25%, and those of Scheduled Castes and Scheduled Tribes from 16% to 20% and 1% to 2%, respectively. This took the total reservation level to 65%. Applying judicial precedents that have now crystallised into a legal bar on reservations exceeding 50%, the court has inflicted a huge blow to the Bihar government’s plan to utilise its Caste Survey findings to expand its affirmative action programme. The government may have erred in its policy approach — armed with caste-wise population numbers — when its preamble to the amending law said it aimed to achieve “proportionate equality”. The court agreed with the petitioners challenging the increased quotas on a key point: that adequate representation does not mean ‘proportionate representation’, as clarified in the famous nine-judge verdict in Indra Sawhney (1992). If any attempt to raise the quota level earmarked for any section to be in proportion to the State’s population results in the total reservation percentage exceeding the permissible limit, it is liable to be unconstitutional.
However, it is unfortunate that the court was so zealous about the reservation ceiling, that it rejected the State’s argument on the existence of special circumstances. Indra Sawhney did allow the quota ceiling to be exceeded in “extraordinary situations”. It suggested that the population living in remote or far-flung areas may require to be treated in a different way. The court seems to have taken that geographical remoteness is the only special situation to justify an enhanced quota and denied the benefit to Bihar. It is difficult to believe that a State which is backward in most parameters of human and social development should be denied the use of its executive and legislative power to expand its social justice programme. The court surely saw merit in the argument that there was no in-depth study before enhanced reservation was implemented. This raises the question whether the survey was indeed quite exhaustive when it gave a caste-wise break-up of the population and their economic conditions. While there may be a case for pruning the BC or EBC list based on the progress made over the last few decades, it might not be just to stymie every attempt to enhance the numerical representation of historically deprived sections on the ground that it exceeds the quota ceiling.
देशहित में एक राष्ट्र-एक चुनाव
केसी त्यागी, ( लेखक जदयू के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद हैं )

देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने 18,626 पृष्ठों की रिपोर्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया है। यह रिपोर्ट इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनावों को भी एक साथ कराने की वकालत करती है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय विधि आयोग के समक्ष सरकार के इन विधायी प्रयासों का समर्थन किया था। ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ अवधारणा भारत में संसदीय, राज्य और स्थानीय सहित सभी चुनावों को एक निश्चित अंतराल, आमतौर पर हर पांच साल में आयोजित करने की वकालत करती है। भारतीय राजनीति में एक साथ चुनाव कराने का यह विचार नया नहीं है। इससे पहले 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने की वजह से पहली बार एक साथ चुनाव होने का चक्र बाधित हुआ था। वहीं चौथी लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई थी, जिसकी वजह से 1971 में नए चुनाव हुए। एक साथ चुनाव का विचार पहली बार औपचारिक रूप से भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी 1983 की रिपोर्ट में प्रस्तावित किया था। बाद में भारत के विधि आयोग ने भी इसका समर्थन किया।
लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार को अमल में लाना देशहित में है। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष की चिंता है कि मौजूदा सरकार अपने प्रभाव और महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के जरिये लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को प्रभावित करने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में स्थानीय मुद्दे गौण हो सकते हैं, लेकिन यह भय व्यर्थ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन उसके तुरंत बाद कई विधानसभा चुनावों में उसे पराजय मिली। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा में भाजपा को सात सीटों पर मिली बढ़त और विधानसभा में बीजद को बहुमत मिलना भी यही जाहिर करता है। दरअसल देश और प्रदेशों के अपने-अपने मुद्दे संबंधित चुनावों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इस बार के लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह राशि किसी दल की नहीं, बल्कि भारत सरकार के कोष में संचित देश के करदाताओं की है। एक साथ चुनाव से रैलियों, रोड शो, लोकलुभावन व्यय समेत बूथ और अन्य प्रबंधकीय खर्चों में कई गुना कमी आएगी। इससे करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल विकास कार्यों में हो पाएगा। बार-बार चुनाव होने से उम्मीदवारों द्वारा वहन किया गया अतिरिक्त खर्च भी देश में काले धन के प्रवाह को गति देता है। एडीआर के अनुसार राजनीतिक दलों के कुल चंदे का लगभग 70-80 प्रतिशत हिस्सा अज्ञात स्रोतों से आता है। मौजूदा चुनावी संरचना में हर साल देश का कोई न कोई राज्य चुनाव में व्यस्त रहता है। इसके चलते चुनावी आचार संहिता लागू हो जाने से सरकार और मतदाता दोनों के रोजमर्रा के कार्य प्रभावित होते हैं। इस दौरान न तो कोई नई नीतिगत घोषणा हो पाती है, न ही उसका क्रियान्वयन। मंत्रियों समेत प्रशासनिक अधिकारियों की चुनावी प्रक्रिया में व्यस्तता की वजह से विकास और जनकल्याण के कार्य ठप रहते हैं।
हालांकि तमाम अनुशंसाओं के बावजूद एक साथ चुनाव की व्यवस्था करना आसान नहीं है। इस दिशा में एक सवाल यह है कि बहुमत की सरकार यदि अल्पमत में आ जाए तो उस स्थिति में विकल्प क्या होगा? इस स्थिति में नि:संदेह पुनः चुनाव की कवायद प्रचलन में है। एक साथ चुनाव कराने के लिए भंग लोकसभा या विधानसभा को शेष अवधि तक के लिए स्थगित रखना या फिर बहुमत खो चुकी सरकार का सत्ता में बने रहना भी लोकतांत्रिक जनादेश के लिए अपमानजनक होगा। संविधान के अनुच्छेद-356 के उपयोग तथा उसके बाद की दशा भी चिंता का विषय होगी। जहां तक संविधान में बदलाव कर इस नई व्यवस्था को गति देने का विषय है तो इसमें संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान परिदृश्य में चुनौतीपूर्ण है। इस क्रम में कई राज्य सरकारों की कुर्बानी पांच वर्ष के कार्यकाल से पहले देनी पड़ सकती है। इसलिए प्रस्तावित सिफारिशों के लिए आम सहमति अनिवार्य है। यह पहल ऐतिहासिक है। इसलिए इसकी दूरगामी चुनौतियों को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा।
अब कसेगी नकेल
संपादकीय
सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू कर दिया है। इस एंटी-पेपर लीक कानून के तहत पेपर लीक या उत्तर-पुस्तिका से छेड़छाड़ करने पर कम से कम तीन साल की सजा होगी जिसे दस लाख तक के जुर्माने के साथ बढ़ा कर पांच साल तक भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चार महीने पहले ही लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे चुकी थीं। इस कानून का उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिग भर्ती परीक्षाओं और एनटीए द्वारा आयोजित अन्य तमाम परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना है। इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों पर अब न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून से पहले राज्यों में नकल रोकने और परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली को रोकने संबंधी कानून बनाए गए हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड में ऐसे कानून हैं। हालांकि ये उस तरह के नतीजे देने में असफल रहे हैं, जिनके बलबूते परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जा सके। इस नये कानून द्वारा परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के प्रमुख और सदस्यों को लोक सेवक माना जाएगा ताकि उनके खिलाफ अपराध के साथ ही भ्रष्टाचार का मामला भी चलाया जा सके। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पर उठने वाली उंगलियों के कारण युवाओं का भरोसा लगातार टूट रहा है। बार-बार परीक्षा प्रणालियों पर संदेह और उनकी पारदर्शिता धूमिल पड़ने के चलते प्रतियोगियों में निराशा व्याप्त होती जा रही है। चूंकि अब यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आ गया है, इसलिए कोई भी पुलिस अधिकारी बगैर वारंट भी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। भले ही यह फैसला लेने में सरकार ने काफी ढिलाई बरती है लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद क्योंकि उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए परीक्षार्थियों का समूचा भविष्य ही दांव पर लगा होता है। परीक्षाओं में धांधली होनहार युवाओं को नैतिक तौर पर बुरी तरह तोड़ देती है। हालांकि सख्त कानून बनाने में वक्त लगता है। विशेषज्ञों की राय और विभिन्न दृष्टिकोणों से इसे उस सख्ती से लागू किया गया ताकि भविष्य में इस तरह का कोई संकट ही न खड़ा हो सके। साथ ही, इस तरह के अपराधियों पर लगाम कसी जा सके। देखा जाना है कि कानून सख्त किए जाने के बाद पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधलियों पर नकेल कसने में हम किसने सफल होते हैं।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नीति और नियम जापान से सीखे भारत
जसप्रीत बिंद्रा, ( तकनीक विशेषज्ञ )
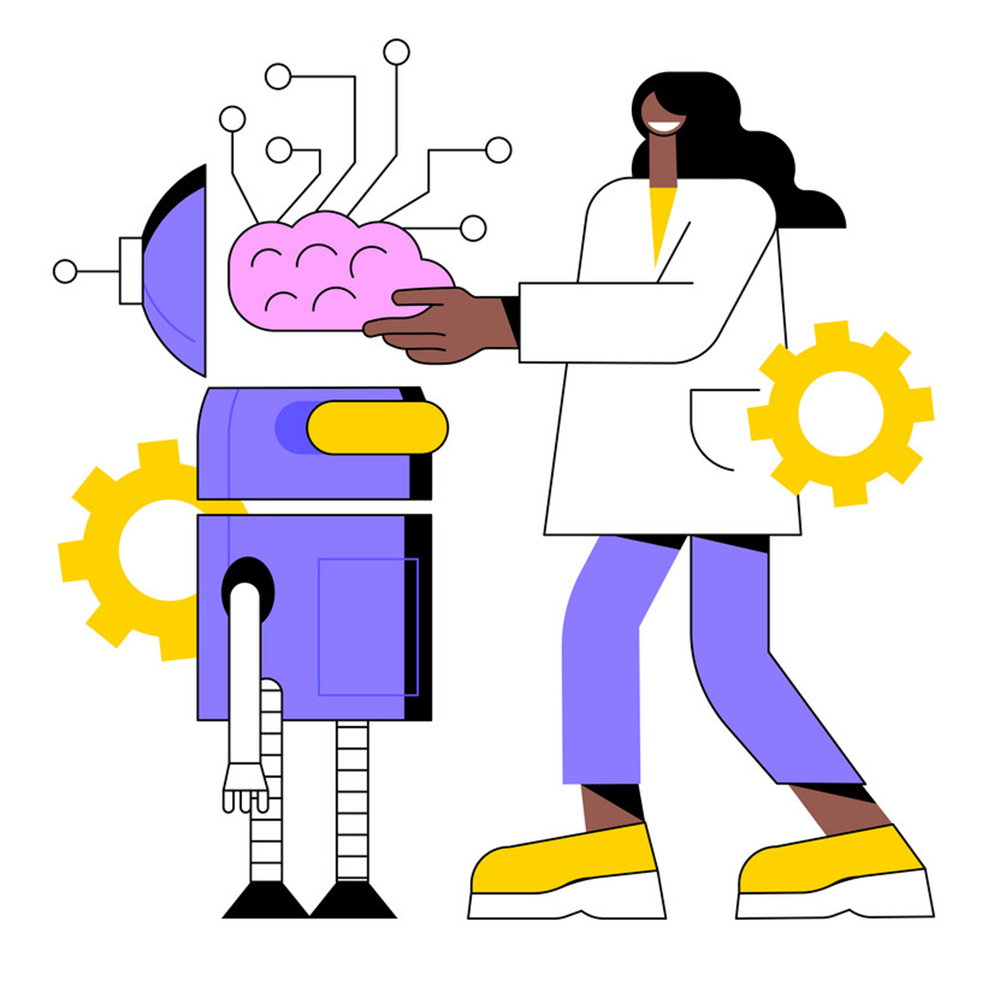
मेरा मानना है कि भारत को पूर्व की ओर देखना चाहिए और जापान से सीखना चाहिए, जो ऐसे नियम बना रहा है, जिसमें नवाचार का माहौल बनाने के साथ-साथ सुरक्षित एआई के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। उसकी नजर में एआई ऐसा प्रेरक है, जो नवाचार और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में दशकों से आए ठहराव को दूर कर सकती है। 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनने के लिए हम भी एआई से इसी तरह मदद ले सकते हैं। दरअसल, जापान ने 2023 के जी-7 शिखर सम्मेलन का फायदा उठाया, जिसमें ‘हिरोशिमा एआई प्रोसेस’ (एआई सिस्टम बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमन को बढ़ावा देने वाला फ्रेमवर्क) द्वारा एआई को विनियमित करने के लिए प्रावधान बनाने पर जोर दिया गया। इसमें दो दृष्टिकोण सामने आए- पहला, यूरोपीय संघ या चीन के नियमों की तरह सख्त कानून बनाया जाए, और दूसरा, पारंपरिक सिद्धातों और निगरानी को दरकिनार करके अपेक्षाकृत नरम कानून बनाना। जापान ने दूसरा नजरिया चुना।
स्टेलेनबोश यूनिवर्सिटी की इंगे ओडेन्डाल ने अपने शोध-पत्र में उसके प्रयासों के बारे में बताया है। इनमें पहला है, सरकार का सुविधा-प्रदाता के रूप में काम करना- जापान की सरकार नवाचार से जुड़े प्रयासों को अपनी मुट्ठी में कैद करने के बजाय उसके लिए सुविधा मुहैया कराने वाली संस्था बनना पसंद करती है। वह निजी क्षेत्र को अगुवा मानती है और अपने विभागों को उनकी मदद के लिए सक्रिय रहने को कहती है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमारी सरकार को निजी क्षेत्र को केंद्र में रखना चाहिए और तमाम मंत्रालयों के माध्यम से सहयोगी भूमिका निभानी चाहिए। दूसरा है, वित्तपोषण और निवेश पर ध्यान- जापान ने जेनरेटिव एआई, घरेलू डाटा सेंटर और स्थानीय चिप उत्पादन के लिए एक बड़ा कोष बनाया है। इससे तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी में प्रोत्साहन व सब्सिडी प्रदान की जाती है। भारत में भी इस तरह का कोष है, जो इंडिया एआई योजना के तहत बना है। मगर अंतर यह है कि इसका उपयोग प्रसंस्करण इकाइयों की खरीद पर अधिक हो रहा है, न कि जापान की तरह नवाचार पर।
तीसरा है, सरकार, अकादमिक और उद्योग में सामंजस्य- ‘एआई जापान आरऐंडडी नेटवर्क’ देश के तमाम विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, निजी क्षेत्र व वैश्विक तकनीकी कंपनियों के साथ मिलकर एआई शोध और कंपनियों से जुड़ी नीतियों की सिफारिश करता है। भारत भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। मजबूत निजी क्षेत्र के साथ-साथ वैश्विक तकनीक में हमारा खास दखल है। चौथा है, घरेलू क्षमता का निर्माण- जापान अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) बनाने की सोच रहा है। भारत में भी ऐसे कई मॉडल बन रहे हैं और उनको सरकारी मदद से लाभ होगा। आधार, यूपीआई जैसे कदमों से पता चलता है कि आम लोगों को केंद्र में रखकर हम तकनीक विकसित कर सकते हैं। इसी तरह जेनरेटिव एआई को आम जनजीवन में उतारा जा सकता है। और पांचवां है, दार्शनिक नजरिया- निजता और डाटा उपयोग जैसे बुनियादी मसलों पर पूरब और पश्चिम की सोच अलग है। पश्चिमी देशों के लिए जहां निजता का अर्थ है, अकेले रहने का अधिकार, वहीं पूरब में इसका मतलब है, सामूहिक व सामाजिक निजता। ऐसे में, हमें एआई नियमन को लेकर उचित ही जापान की ओर देखना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति मिलती है और जो नवाचार व नियमन को लेकर संतुलित नजरिया भी रखता है।