
21-10-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
No Plan is a Terrible Plan for Our Cities
ET Editorials
India is poised for a remarkable transformation. Its urban population is projected to surge from today’s 450 million to a staggering 800 million in the next 25 years. Urban GDP is expected to rise from 60% to 80%. But there is one big problem: most of our cities are not prepared for the future. Bengaluru-based think tank Janaagraha’s 2023 Annual Survey of India’s City-System finds about 39% of state capitals lack active master plans, essential blueprints that guide urban development over the next two decades. A 2021 NITI Aayog report highlights that nearly 65% of urban settlements, including census towns, lack master plans, resulting in unsustainable urban sprawls marked by disjointed interventions, haphazard construction and rampant environmental pollution. This is bad news for an aspiring ‘developed country’.
Three core issues can be attributed to the looming crisis: a severe shortage of skilled urban planners, financial constraints and limited powers of local governments. While India would require 300,000 urban planners by 2031, it now has about 5,500. It has about 8,000 cities and towns, 600 districts and over 400,000 villages, compounding the planning challenges. Also, most cities generate only a fraction of their revenue, relying heavily on central and state governments. Local governments lack autonomy and are often restricted from performing their constitutionally mandated duties. The absence of empowered mayors exacerbates this problem.
Urbanisation is intrinsic to development and economic growth. So, getting a fix is a must. It is also imperative that development plans are insightful, adaptable and responsive to evolving needs, and integrate views of citizens. Only then can India’s cities be adequately future-ready.
The politics of a caste census, its impact on secularism
A caste census could trigger a process of social engineering that could upset Hindutva’s apple cart of Hindu majoritarian unity
Shaikh Mujibur Rehman teaches at Jamia Millia Central University, New Delhi
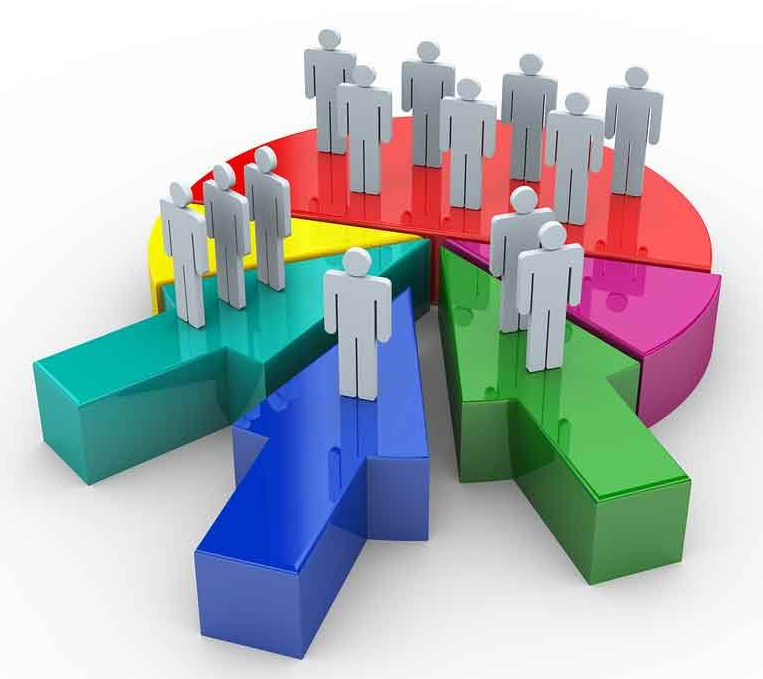
According to scholars who work on Indian poverty, there are two kinds of poverty, i.e., economic and institutional. Caste plays a pivotal role in the perpetuation of institutional poverty because, historically, it determines occupation and skills. In the modern Indian economy, most occupations are network driven in which caste plays decisive roles in driving those networks, which is why a caste census is vital. This is also why Rahul Gandhi’s observation that such a census ‘is like the X-ray of India’ makes some sense. By not recognising that caste has bred poverty, Mr. Modi is turning a blind eye to a deeply painful reality of Indian society. It is not just Mr. Modi, but even the trickle down approach of the Nehruvian model, which economist Sukhamoy Chakravarty used to describe as the Nehru-Mahalanobis model of development did not recognise either. Therefore, non-recognition of the organic relationship of caste and poverty has been a long neglected fact of Indian policy thinking.
Explaining the right’s reluctance
However, the reason why Hindutva seems reluctant to have a caste census is because it believes it might open a Pandora’s box of claims and counter-claims relating to positions and power — about who got what, when and how. Such a census would serve as the enduring source for divisive politics and trigger a never-ending process of social engineering that would upset Hindutva’s apple cart of Hindu majoritarian unity, which it has stitched together after decades of hard work through intense grass-root campaigns.
Utilising the politics of religious polarisation, Hindutva forces are within striking distance of fulfilling their political dream of Hindu majoritarian unity, which appeared almost Utopian in the mid-1970s. On the other hand, secular political groups are also aware of the divisive potential of a caste census. For them, it is the most potent weapon among others to contain the growing electoral influence of Hindu majoritarian forces.
Looking at caste-based politics in Uttar Pradesh, it was argued that assertions of caste identities would help in a secularisation of the Indian polity. This appeared to have borne fruit during the period when the Samajwadi Party (SP) and Bahujan Samaj Party (BSP) were coalition partners, and the Bharatiya Janata Party was contained in Uttar Pradesh. However, there has been no guarantee of its continuation as subsequent political developments since 2014 have shown, where there has been an unprecedented resurgence of Hindutva politics in the heartland. While secularisation could be a possibility, there is also an alternative possibility in which caste fragmentation or caste-inspired social engineering and Hindu majoritarianism could grow in tandem, creating a new model for competitive Hindutva politics. Therefore, the prospect for the revival of secular politics owing to a caste census is rather limited. It is a gamble from the point of view of a resurrection of secularism in India. It might contain the pace of Hindutva politics but is not the ultimate outcome that may lead to the establishment of a Hindu majoritarian political culture or a similar variant of state.
The last time that a caste census was carried out was in 1931, a time when organised right groups were marginal players during India’s freedom movement. After Independence, there was a possibility for a caste census to be resumed in 1951. It is plausible that in the non-resumption of caste census in 1951, the right might have played a crucial role. Because, as Bruce Graham, author of a most definitive work on the Bharatiya Jana Sangh (BJS) has argued, the right was deeply embedded in secular political formations, particularly in the Congress party. It will not be far-fetched to argue that there might be some overlap in the reasons behind why the word “secular” despite some effort was not included in the Indian Constitution, and the reason why a caste census was not resumed in 1951. Embedded right groups might have played their part at the time in their concerted resistance to India’s secular project. The present-day resistance only echoes the same old reasoning but is much louder in volume, and more organised.
चुनावी बॉन्ड के तमाम पहलुओं पर गौर करे कोर्ट
संपादकीय

समलैंगिक विवाह का जटिल सवाल
डा. ऋतु सारस्वत, ( लेखिका समाजशास्त्री हैं )
हाल में उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इन्कार कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि इस बारे में कानून बनाने का काम संसद का है। हालांकि पीठ ने इस पर जोर दिया कि समलैंगिक व्यक्तियों को अपना साथी चुनने का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि 6 सितंबर, 2018 को समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर कोई आदेश पारित करने के स्थान पर इस बारे में संसद को विचार करने को कहा। आशा की जाती है कि संसद समलैंगिक लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए समाज और परिवार संस्था को ध्यान में रखकर ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। ध्यान रहे कि शीर्ष अदालत के फैसले को समलैंगिक संगठन अपने मानवाधिकार का हनन कह रहे हैं। उनके द्वारा यह स्थापित करने की चेष्टा की जा रही है कि वे विषम-लिंग दंपतियों की ही भांति हैं और उन्हीं की तरह अच्छे अभिभावक भी बन सकते हैं। अपने इस तर्क के पीछे वे कुछ सामाजिक शोधों को आधार बनाते हैं, परंतु कई समाजशास्त्री तथा मनोविज्ञानी यह कहते रहे हैं ऐसे शोध अधिकांशतः अधिवक्ताओं द्वारा ही किए गए हैं, जो सामाजिक वैज्ञानिक शोध की प्रविधियों से अमूमन परिचित नहीं होते, इसलिए ये शोध त्रुटियों से ग्रस्त हैं। इस संबंध में सबसे गहन समीक्षा समाजशास्त्र के प्रो. स्टीवन नाट द्वारा की गई। उन्हें कनाडा के अटार्नी जनरल के विशेषज्ञ गवाह के रूप में कई सौ ऐसे अध्ययनों की समीक्षा करने के लिए कहा गया था, जो समलैंगिकता को उभयलिंगी संबंधों के समतुल्य मानते हैं। स्टीवन ने निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा समीक्षा किए गए सभी शोधों में निष्पादन की कम से कम एक गंभीर कमी थी। उनमें से एक भी अध्ययन वैज्ञानिक अनुसंधान के सामान्य स्वीकृत मानकों के अनुसार आयोजित नहीं किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये तमाम अध्ययन उस तरह का सामाजिक, वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते, जिनके आधार पर संपूर्ण वैवाहिक एवं पारिवारिक संस्था में बदलाव किया जाए।
इस महत्वपूर्ण तथ्य पर चिंतन करना आवश्यक है कि सभ्यता की परिपक्वता के बाद से ही विवाह और प्रजनन एक-दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, जिस पर समान-लिंग विवाह सीधे तौर पर आघात करेगा। वास्तव में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवाह का प्रारंभिक उद्देश्य जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को माता-पिता, दोनों का ही सान्निध्य और सुरक्षा प्राप्त होना है। समाज का एक वर्ग विवाह को भावनात्मक जुड़ाव के रूप में ही देखता है। किसी भी देश विशेष की जनसंख्या में कमी उस पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दबाव डालती है। समान लिंग विवाह केवल विवाह से लंबे समय से जुड़े प्रजनन मानदंड को ही कमजोर नहीं करेगा, बल्कि यह भी स्थापित करेगा कि प्रजनन और विवाह के बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है। यह कोई संयोग नहीं कि जिन देशों ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है, वहां प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है। समलैंगिक जोड़े दावा करते रहे हैं कि समलैंगिकता प्राकृतिक या जैविक है, परंतु इस दावे से इतर समलैंगिक संबंधों पर बहुचर्चित पुस्तक ‘होमोसेक्सुअलिटी एंड द पालिटिक्स आफ ट्रुथ’ के लेखक डा. जैफरी सतिनोवर कहते हैं कि उन्होंने उन अनेक दावों की जांच की, जो यह कहते हैं कि समलैंगिकता प्राकृतिक एवं स्वाभाविक है। सतिनोवर ने पाया कि इनमें से कई अध्ययन त्रुटिपूर्ण हैं। समलैंगिक संबंधों पर अपने दो दशकों से भी अधिक के शोध के पश्चात वह कहते हैं कि समलैंगिकता स्थायी या जैविक प्रकृति नहीं, अपितु यह परिवर्तनशील है। वह बताते हैं कि कैसे मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, पसंद और आदत सभी आपस में जुड़कर यौन व्यवहार के गहरे अंतर्निहित स्वरूपों का निर्माण करते हैं। समलैंगिक संबंधों पर सतिनोवेर का अध्ययन आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान, आदतों की समझ, लत और दबाव की अवधारणा पर केंद्रित है। सतिनोवर की पुस्तक इस पर विचार करने को विवश करती है कि कैसे निरंतर यह अवधारणा स्थापित करने की चेष्टा की गई है कि समलैंगिक संबंध उभयलिंग संबंधों की ही भांति हैं।
समलैंगिक कार्यकर्ताओं ने पिछली सदी के सातवें दशक में अमेरिकियों को यह समझाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया कि समलैंगिकता सामान्य है। यह अभियान जल्द ही विश्व भर में फैल गया। किक तथा माडसेन की पुस्तक ‘आफ्टर द बाल’ के आधार पर समलैंगिक संगठन सामान्य जन को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करने लगे कि समलैंगिकता सामान्य, जन्मजात तथा अपरिवर्तनीय है। समान लिंग विवाह की पैरवी करने वाले सामाजिक परिवर्तन के अवांछित वेग में तर्कहीनता के आधार पर सिर्फ इसलिए बह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए समाज के परंपरागत स्वरूप गौण हैं। वे इस सत्य को विचारने के लिए तैयार नहीं कि समान लिंग यौन संबंध स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होते हैं। डा. सतिनोवेर बताते हैं कि समलैंगिक अपने जीवनकाल के 25 से 30 वर्ष खो देते हैं, जिसका कारण गोनोरिया, क्लैमाइडिया, सिफलिस, हर्पीस, एचआइवी/एड्स, अन्य यौन संचारित संक्रमण और आंत्र संक्रमण आदि हैं। समान लिंग विवाह को मान्यता देने का एक खतरा यह है कि उभयलिंगी दंपतियों को यह संदेश जाएगा कि समाज पितृविहीन या मातृविहीन परिवार की रचना के लिए तैयार है। समलैंगिक विवाह को सामान्य सिद्ध करने में एक ऐसा दबाव समूह कार्य कर रहा है, जो यह समझता है कि समाज में स्त्री-पुरुष के संबंधों का कोई औचित्य नहीं है। ठीक वैसे जैसे कई कट्टर नारीवादी मानते हैं कि पुरुषों की समाप्ति के पश्चात ही स्त्री सशक्त होगी।
