
18-07-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:18-07-23
Date:18-07-23
Gently Pushing Rupee
Steady steps promoting rupee-based foreign trade are pragmatic. Internationalisation follows economic heft
TOI Editorials
On July 15, RBI and the Central Bank of UAE signed two MoUs allowing bilateral trade in their respective domestic currencies. To contextualise this development, go back to two other events where RBI, in conjunction with GOI, tried to internationalise the rupee. In July 2022, it authorised banks to enable international trade settlement in rupees. Separately, in February 2023, India and Singapore linked their fast payment systems UPI and PayNow. This linkage allowed transfer from India of up to ₹60,000/day. Its primary benefit is that it allows a significant reduction in transaction costs of remittances.
India is the world’s largest recipient of foreign remittances. In 2022, the World Bank estimated that India was the first country set to receive an annual remittance flow of more than $100 billion. RBI’s efforts to link its digital payments systems to other central banks provides a boost to remittance flows and the savings in transaction costs benefit recipients. The UAE tie-up, however, is greater in scope and ambition. It aims to promote settlement of all current account trades and permitted capital account transactions in respective domestic currencies. To operationalise it, both central banks have to jointly create a settlement system and develop a rupee-dirham foreign exchange market.
It’s a step towards internationalising the rupee and is in keeping with the growing size of India’s economy and its share in world trade. These efforts come in the backdrop of the dominance of the US dollar in all aspects of trade and foreign currency reserves. About half the global trade is invoiced in USD, almost 60% of official reserves are held in it and it accounts for almost 90% of global foreign exchange transactions. It makes USD the “vehicle currency” for the global forex market. Typically, about 80% of India’s foreign trade is invoiced in USD.
Internationalisation of the rupee requires freer convertibility, deeper and more sophisticated financial markets and a bigger footprint in global trade. Consequently, enabling conditions for the rupee’s internationalisation need to be in sync with the larger trade and macroeconomic policy. Without synchronisation, there will be risks to macroeconomic stability. Therefore, RBI’s gradual approach is pragmatic as it allows retail transactions at a lower transaction cost. Moreover, wherever possible, rupee settlement of cross-border trades is encouraged. Enhanced internationalisation requires GOI to revisit its restrictive foreign trade and capital account policies.
A common civil code spelling equality for every Indian
There needs to be a universal civil code applicable to all Indians, irrespective of faith, gender and sexual orientation
Pulapre Balakrishnan, [ Writer is an economist ]
The 22nd Law Commission has called for responses to a proposal for a Uniform Civil Code in India. This has set off a debate, which has often been acrimonious. But the debate itself is much needed as Indians have never been consulted on the personal laws they are governed by. These laws were instituted by the British colonial government by giving a cursory hearing to the clergy, or religious scholars in the case of religions without one. The result was a religion-based set of personal laws for Hindus, Muslims and Christians. Whether the colonisers did this out of a deep concern for the sentiments of the natives or it was intended as another instrument in a strategy of divide and rule in order to hold India is irrelevant, but we should note the provenance of India’s personal laws.
Laws that are boxed
Personal laws in India are boxed according to the religion or social origins of the citizen. However, it does not take much to see a fearful symmetry between them. This is their unmistakably patriarchal framing, whereby men are privileged at every turn. Thus, only a man can be the ‘karta’ or head of a Hindu Undivided Family, a divorced Muslim woman is not entitled to maintenance beyond a certain period, among some tribes of India, the custom is that women do not inherit ancestral property, and a Parsi woman who marries outside the community is excommunicated. So, from the point of view of women’s empowerment, India’s civil code is uniform already. As for the section of the population that we today refer to as the LGBT community, the British colonialists considered them mere flotsam and jetsam, to be ignored altogether. Not only did they not even merit a personal law but their actions deserved to be criminalised, even when they were consensual.
We can now see why we cannot consider ourselves to be a democracy so long as we continue with current approach to personal law. It is not because it is not the same for different religious groups but because their uniformly patriarchal core denies women equality before the law. Prime Minister Narendra Modi’s widely reported query as to how one country can be run on two laws misses this. But so does the Opposition when it rushes to defend inaction on these personal laws on grounds of diversity, which they hold as sacrosanct.
The antiquity of India’s customs and the diversity of its peoples are both brought up to make a case for tip-toeing around the existing personal laws despite their unequal rights for men and women. But is this a valid argument at all? India’s caste system is antique alright, but India’s lawmakers were wise enough to junk it in law very early on the history of independent India.
The matter of diversity
Next comes diversity. Opponents of reform seem to be unaware that they are extolling a diversity based on religion. Here it is worth recalling political scientist Pratap Bhanu Mehta’s reminder that India was not conceived of as “a federation of religions”. Similarly, during the deliberations of the Constituent Assembly, B.R. Ambedkar is said to have expressed surprise that religion was being given as much importance when choosing India’s political arrangements. These observations have a bearing on what is being debated today. Whether India’s civil code accords with the diktats of all religions is irrelevant. What matters is that it must be in accord with the democratic principles of liberty, equality and dignity. It is entirely possible to draft a civil code that preserves these ideals without any reference to religious practices. This would have the merit of being secular, in keeping with the defining character of India’s constitution.
Self-appointed heads of religious groups have resisted calls for a common civil code by resorting to the argument that it infringes upon religious freedom. They fail to see that religious freedom means the freedom to adopt the faith of one’s choice. In the domain of expression of faith, such as public worship, Indian courts have declared that it should conform to constitutional principles. In what may be considered one of the most significant social changes in India, restriction of temple entry to the avarna was discontinued almost a century ago. Much later, the Supreme Court of India struck down the practice of restricting women’s entry to the Sabarimala temple.
These milestones point to an understanding of the right to religion as being confined to choice of one’s faith and not to extra-constitutional expressions of it, such as the regulation of women’s autonomy by men. This takes us to the question of the efficacy of legislation in advancing rights. For instance, when it comes to temple entry, we find instances of Dalits being denied entry even today. There are also recorded cases of bigamy among Hindus, in some regions greater than among Muslims. But the conclusion drawn from this that banning polygamy among Muslims is discriminatory is a non sequitur. The response to finding bigamy among Hindus hardly invalidates a call for ending the provision for polygamy among Muslims. The right response would be to prosecute those Hindus violating the law.
What is relevant here is not parity among men of different religious groups when it comes to marriage, it is the rights of women within every religious grouping. The demand that sections of the population, whether tribal or Muslim, are entitled to separate personal laws even when they are gender unjust fails to acknowledge that they are equal beneficiaries of India’s democracy. Democracy guarantees them liberty and equality in all spheres of life, including access to the rule of law, freeing them from arbitrary governance. A reform of their personal laws to end gender discrimination, rendering them compatible with democracy, would be no more than to seek a balance between their rights and their responsibilities.
Bridging a gap
The obsession with parity among males across India’s religion-based personal codes blanks out the issue of the rights of its LGBT community. No amount of reform of the Hindu, Muslim and Christian personal codes can reach them, for they have been rendered invisible by these colonial-era constructions. If there were to be a common civil code applicable to all Indians irrespective of faith, gender and sexual orientation, the LGBT population could be accommodated within it. In its absence, an alternative would have to be conceived of. Given the recognition implicitly granted to them with the reading down of Section 377 of the Indian Penal Code in 2018 and a highly visible hearing of a petition in the Supreme Court to allow same-sex marriage, which concluded only recently, the question of a personal law for this group can no longer be postponed.
To be credible, the current debate on personal law must include the LGBT, for the questions of civil partnership, inheritance and adoption are as relevant to them as to other Indians. Mundane acts such as opening a bank account or purchasing life insurance would make one aware of this. Complacently confining the discussion of India’s personal laws within a Hindu-Muslim binary, leaves unrecognised the potential to empower a wide section of the population through their drastic overhaul. The combination of uniformly gender unjust personal laws and a disempowered LGBT population points to the advantage of having a universal civil code which encompasses all Indians. On Independence Day in 1947, Prime Minister Jawaharlal Nehru had, in a message to the nation, stated that the task before India was to “create social, economic and political institutions which will ensure justice and fullness of life to every man and woman”. No social cleavage has been imagined in this vision. A universal civil code would be a step in that direction.
विकास की सतत प्रक्रिया ही प्रजातंत्र की खूबी है
संपादकीय
यूएनडीपी के ताजा बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के अनुसार भारत में वर्ष 2005-06 में जहां 64.50 करोड़ गरीब थे, वहीं वर्ष 2015-16 में ये संख्या घटकर 37 करोड़ रह गई, जो कि वर्ष 2019-21 में 23 करोड़ पर आ गई। 15 वर्षों में कुल 41.50 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर हुए और शिशु मृत्यु दर एक-तिहाई रह गई। प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में लोक-कल्याण एक सतत प्रक्रिया है और जो सरकार इसे नजरअंदाज करती है या जन- अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती, वह सत्ता से बाहर हो जाती है, बशर्ते जनता के पास विकल्प उपलब्ध हो। लिहाजा सरकारों पर लगातार बेहतर परफॉर्म करने का दबाव बना रहता है। यूएनडीपी ने वर्ष 2010 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पाया कि गरीबी की अवस्था किसी एक सूचकांक से तय नहीं की जा सकती, लिहाजा इसके आकलन के लिए उस व्यक्ति या परिवार के पास शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के अलावा जीवन स्तर के तमाम इंडीकेटर्स बनाए गए। खाना पकाने के लिए गैस, स्वच्छ पानी, स्कूल टाइम, पोषक तत्वों की उपलब्धता आदि कई नए पैरामीटर्स पर इसका आकलन किया गया। ताजा आंकड़ों से यह भी पता चला कि तेजी से बहु-आयामी गरीबी कम करने वाले देशों में भारत के साथ चीन, कंबोडिया, कांगो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरोक्को, सर्बिया और वियतनाम भी हैं। बिजली, पेयजल और आवास की उपलब्धता भी बढ़ी है। आजादी के समय देश में 50 मिलियन टन अनाज पैदा होता था जबकि आबादी 36 करोड़ थी। आज अनाज साढ़े छह गुना (320 मिलियन टन) पैदा हो रहा है जबकि आबादी चार गुना बढ़ी है। कुल मिलकर सरकारों को विकास करना ही पड़ता है। देखना यह होता है कि अन्य समकक्ष देश जैसे चीन, इजराइल या जापान का विकास भारत के मुकाबले तेज होने के मूल कारण क्या हैं?
Date:18-07-23
देश से अमीरों का पलायन क्यों हो रहा है?
अंशुमन तिवारी, ( मनी-9 के एडिटर )
रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर (77 ई.) मुजरिस ( कोचीन के निकट) में भारतीय समृद्धि का जलवा देखकर लौटा था। उसने लिखा कि भारत दुनिया के सोने-चांदी की भट्टी बन गया है। सारी रोमन सम्पत्ति खिंचकर वहां जा रही है। ऐसी ही शिकायत ब्रिटेन की मस्कोवी कंपनी के चांसलर एंथनी जेनकिंसन को थी, जो 16वीं सदी के आखिरी दशक में बुखारा के बाजार में भारतीय कारोबारियों को ऊन बेचना चाहते थे। मगर भारतीय सोना-चांदी और महंगे पत्थरों में भुगतान लेते थे। पुर्तगालियों को भी यह तकलीफ सालती रही कि भारत दुनिया भर की समृद्धि खींच रहा है। इन संदर्भों से गुजरते हुए ताजा सुर्खियां हैरत में डाल देती हैं। 21वीं सदी में अब भारत की समृद्धि खिंचकर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जाने लगी है। यह काला धन नहीं है। यह तो उद्यमियों की जायज सम्पत्ति है, जो उन्होंने भारत से कमाई है लेकिन इसका निवेश दूसरे देशों में हो रहा है।
हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट (जून 2023 ) ने बताया कि 2023 में लगभग 6500 अल्ट्रा रिच भारत छोड़ देंगे। बीते साल करीब 7500 ऐसे ही अमीरों ने भारत को अलविदा कहा था। ऐसे लोगों के लिए हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स (एचएनडब्लूआई) शब्द का इस्तेमाल होता है। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के पास 10 लाख डॉलर से ज्यादा की निवेश योग्य सम्पत्ति होती है। इसका मतलब है शेयर, प्रॉपर्टी या नकद में निवेश का आकार एक मिलियन डॉलर से ज्यादा। इसमें कर्ज शामिल नहीं है।
अमीरी की नापजोख : भारत छोड़कर जाने वाले इन सुपर रिच की संख्या छोटी नहीं है। भारत के पास 1 मिलियन डॉलर से अधिक निवेश योग्य सम्पत्ति वाले लोग हैं ही कितने ? क्रेडिट सुई की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट पूरी दुनिया में समृद्धि की नापजोख करती है। इस रिपोर्ट का 2022 का संस्करण बताता है कि 2021 में दुनिया की कुल वेल्थ करीब 463.6 ट्रिलियन डॉलर थी । उत्तरी अमेरिका और चीन करीब 89 फीसदी ग्लोबल सम्पत्ति की मेजबानी करते हैं। यूरोप, भारत, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का संयुक्त हिस्सा 11.1 फीसदी है। क्रेडिट सुई ने ग्लोबल वेल्थ पिरामिड के मुताबिक 1 मिलियन डॉलर से ऊपर के वर्ग में केवल 1.2 फीसदी वयस्क लोग आते हैं। इनकी कुल संख्या 6.2 करोड़ है। इनके पास दुनिया की करीब 48 फीसदी वेल्थ है, जो 221.7 ट्रिलियन डॉलर है। हेनली की रिपोर्ट इन्हीं 1.2 फीसदी लोगों के प्रवास के बारे में बताती है। इसलिए इन परम धनिकों के छोटे-से समूह में में 6500 लोगों का भारत छोड़ना बहुत मायने रखता है।
चल हंसा उस देस : बीते छह-सात वर्षों से भारत समृद्धि का निर्यात कर रहा है। एफ्रेशिया बैंक के ग्लोबल माइग्रेशन रिव्यू 2018 के मुताबिक समृद्धि गंवाने वाले मुल्कों में चीन और रूस के बाद भारत तीसरे नंबर पर था । 2017 में करीब 7,000 भारतीय सुपर रिच विदेश में बस गए थे। मोर्गन स्टेनले ने 2016 में बताया था कि 2014 के बाद करीब 23,000 समृद्ध लोग या परिवार भारत छोड़कर विदेश में जा बसे हैं। हेनली की रिपोर्ट के अनुसार औसतन 7000 व्यक्ति- जिनके पास निवेश के लिए एक मिलियन डॉलर से ज्यादा हैं- हर साल भारत छोड़ रहे हैं। 2022 के अंत में भारत में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 3.44 लाख थी। 1078 लोग सेंटी मिलियनेयर थे यानी जिनकी वेल्थ 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा हो। 123 लोग बिलियनेयर थे यानी एक अरब डॉलर (करीब 8200 करोड़ से ज्यादा) निवेश योग्य सम्पत्ति वाले लोग।
अमीरों के नए डेरे : अल्ट्रा रिच का अंतरराष्ट्रीय प्रवास सम्पत्ति के नए ठिकाने भी बताता है। चीन और भारत के अलावा ब्रिटेन, रूस, ब्राजील और हांगकांग से सुपर रिच अपना बोरिया-बिस्तर बांध रहे हैं। उनके नए पते अब ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड में दर्ज हो रहे हैं। हर साल यहां से करीब 1200-1300 धनाढ्य यूरोप में बस रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का जलवा कायम है। 2022 में करीब 3500 अल्ट्रा रिच ने कंगारूओं के मुल्क को अपना ठिकाना बनाया। 2019 में यहां ऐसे 12000 लोग आए थे। न्यूजीलैंड में भी 800 से 1000 अल्ट्रा रिच हर साल पहुंच रहे हैं। सिंगापुर बड़ा आकर्षण है। 2019 से 2022 तक करीब 4300 सुपर रिच यहां डेरा जमा चुके हैं। चीन के अमीर यहां बस रहे हैं। हांगकांग भी अपनी समृद्धि सिंगापुर को भेज रहा है। शून्य टैक्स, नया बुनियादी ढांचा, ढेर सारी सुविधाओं के साथ अरब के मुल्क नया आकर्षण हैं। हेनली रिपोर्ट ने बताया है कि 2023 में करीब 4000 सुपर रिच यहां आ बसेंगे। रूस और भारत के अल्ट्रा रिच खाड़ी के देशों में बस रहे हैं।
भारत क्यों हुआ बेगाना : भारत में एक तरफ दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था का यशोगान चल रहा है, दूसरी तरफ अंबानी-अदाणी भी सिंगापुर या दुबई में फैमिली ऑफिस खोल रहे हैं। सरकार को नए नियम बनाकर इन पर सख्ती करनी पड़ी है।
सम्पत्ति का यह पलायन नीरव मोदी, विजय माल्या या मेहुल चोकसी जैसा आपराधिक नहीं है, बल्कि वैध समृद्धि का सुविचारित प्रवास है। भारत छोड़कर जाने वाले सुपर रिच अपना कारोबार बंद नहीं कर रहे हैं। वे यहीं से सम्पत्ति कमाएंगे। टैक्स भी देंगे। लेकिन निवेश योग्य निजी सम्पत्ति को किसी ऐसे देश ले जा रहे हैं, जहां टैक्स कम है। या निवेश पर बेहतर रिटर्न के वैध रास्ते उपलब्ध हैं। ऊंचे टैक्स की मार से अमीरों का देश छोड़ना नीतिगत विफलता है। सरकार इनकी सम्पत्ति को संजोने, निवेश करने या उपभोग के अवसर ही नहीं बना पाती, ताकि भारत से कमाया पैसा भारत में ही रहे।
गंभीर खतरों का सामना करता हिमालय
अनिल प्रकाश जोशी, ( लेखक पर्यावरणविद् और हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं )
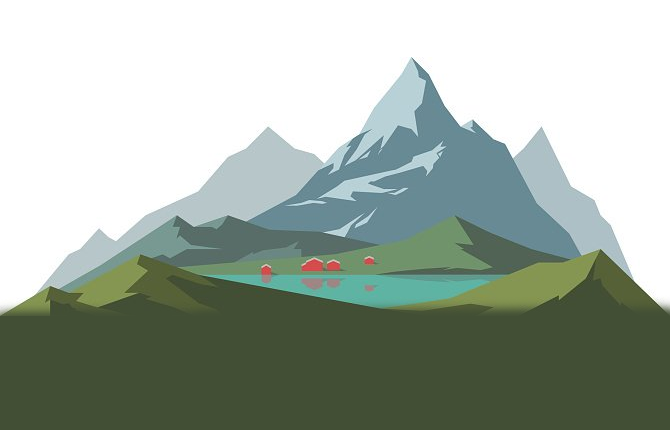
इस बार की बारिश ने एक बार फिर 2013 की त्रासदी की याद दिला दी। तब केदारनाथ की घटना ने जान-माल का बड़ा नुकसान किया था। इस बार की बारिश ने फिर से हिमाचल और उत्तराखंड को पूरी तरह झकझोर दिया है। अब पहाड़ मानसून का स्वागत नहीं करते। स्थानीय लोगों के लिए मानसून का समय संकट भरा हो जाता है। पिछले एक दशक में हर साल हिमालय के किसी न किसी इलाके में बारिश से तबाही होती चली आ रही है। अब यह तबाही राष्ट्रीय चिंता का विषय बननी चाहिए। जिस भूभाग से देश को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवयव मिलते हों, यदि वह संकट में हो तो फिर देश की परिस्थितियों को सुरक्षित नहीं समझ सकते।
हिमालयी राज्यों का गठन आर्थिक असुरक्षा और पिछड़ेपन को दूर करने को लेकर हुआ था। इन राज्यों के गठन का एक उद्देश्य यह भी था कि उनके पिछड़ेपन को दूर करते हुए उन्हें देश की मुख्यधारा से जोड़ा जाए ताकि वहां से पलायन थमे। इस क्रम में उस सवाल की अनदेखी कर दी गई, जो पूरे हिमालय की पर्यावरण सुरक्षा को लेकर था। परिणाम सामने है। आज हिमालय त्रस्त है। आज हमें उन तमाम वैज्ञानिक अध्ययनों का संज्ञान लेना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो चुके हैं। धरती के बढ़ते तापमान ने सबको चिंतित कर दिया है। वैसे तो दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं, जहां किसी न किसी तरह की प्राकृतिक आपदाएं न आती हों। इन्हीं वैज्ञानिक अध्ययनों का मानना है कि आने वाले समय में धरती के बढ़ते तापमान का सबसे ज्यादा असर हिमालयी क्षेत्रों में पड़ेगा। इसका कारण भी साफ है। हिमालय पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हैं। पहाड़ों का हिस्सा कच्चा-पक्का है। एक छोटी सी छेड़छाड़ भी भारी पड़ जाती है। बढ़ते तापक्रम के साथ प्रकृति से छेड़छाड़ का सबसे अधिक असर कहीं दिखाई दे रहा है तो हिमालयी क्षेत्र में। दुर्भाग्य की बात है कि पहले हिमालय के पर्वत आर्थिक असमानता को झेलते थे और अब उन्हें पारिस्थितिकी असमानता ने भी घेर लिया है। हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को पालने वाले लोग ही अब पारिस्थितिकी के दंश को झेल रहे हैं। भिन्न-भिन्न कारणों से पहाड़ जिस तरह टूटते चले जा रहे हैं, उसके कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। पहाड़ी क्षेत्रों की तबाही का असर पूरे देश को झेलना पड़ेगा, क्योंकि अवैध खनन, अनियोजित निर्माण आदि के चलते पहाड़ बंजर हो जाएंगे। इससे वहां से पलायन की प्रवृत्ति को और बल मिलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी हमेशा पहाड़ों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। उत्तराखंड को तो वह अपना घर मानते हैं। केदारनाथ के प्रति उनकी प्रबल आस्था है। वह जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब केदारनाथ आपदा के बाद उन्होंने अपने स्तर पर वहां कार्य कराने की इच्छा प्रकट की थी। उत्तराखंड की तरह हिमाचल से भी उनका खास लगाव है। समय आ गया है कि प्रधानमंत्री हिमालय की स्थिति का संज्ञान लेते हुए वहां के पर्यावरण की स्थितियों की गहन समीक्षा कराएं। हिमालयी राज्यों के पर्यावरण की जैसी अनदेखी हो रही है, उसे देखते हुए यह आवश्यक हो चुका है कि केंद्र सरकार हिमालय की रक्षा के लिए आगे आए। हिमालयी राज्यों की आर्थिकी ऐसी होनी चाहिए, जो पारिस्थितिकी पर केंद्रित हो। पहाड़ अब एक ऐसे माडल के प्रतीक्षा में हैं जो उसे हर तरह से स्थिरता प्रदान कर सकें। हिमालय और वहां के जनजीवन को बचाने की पहल तभी सार्थक सिद्ध हो सकेगी, जब उन कारणों का सही तरह निवारण किया जाएगा, जिनके चलते वे संकट में घिर रहे हैं। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि जोशीमठ में क्या हुआ? जोशीमठ जैसी स्थितियां अन्यत्र भी उभर रही हैं। हिमालयी राज्यों के नीति-नियंताओं के साथ मिलकर एक ऐसी कार्यशैली बननी चाहिए, जो समस्त पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आदर्श बने। यदि आज यह काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में हिमालय एक बड़े खतरे से घिर जाएगा और यदि हिमालय खतरे में पड़ा तो देश भी पर्यावरणीय संकट से ग्रस्त हो जाएगा।
 Date:18-07-23
Date:18-07-23
गलत अभिरुचि
संपादकीय
देश के सेमीकंडक्टर उद्योग को गति देने का सरकार का प्रयास सदिच्छा से भरा हुआ है लेकिन इस प्रक्रिया में करदाताओं के पैसे का ही नुकसान हो सकता है। सरकार ने इस दिशा में दो तरफा प्रयास किए हैं। पहला, उसने बनने वाले सेमीकंडक्टर की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए फाउंन्ड्रीज पर होने वाले व्यय के 30 से 50 फीसदी हिस्से की भरपाई की पेशकश की है। दूसरा, उसने हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर के लिए 55,392 करोड़ रुपये मूल्य की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की है। सन 2022 में घोषित तीसरा तत्त्व है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी डीएलआई। यह घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप और छोटे तथा मझोले उपक्रमों को पांच वर्ष तक वित्तीय मदद की पेशकश करती है। इसका लक्ष्य है सेमी कंडक्टर डिजाइन में शामिल कम से कम 20 घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देना और उन्हें अगले पांच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल करने में मदद करना। सरकार इस योजना के जिस दूसरे चरण पर विचार कर रही है वह है घरेलू चिप डिजाइन कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाना। सरकार का विचार है कि घरेलू डिजाइन कंपनियों को वैश्विक कंपनियों को हिस्सेदारी बेचने से रोका जाए।
चिप निर्माण से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकार को देश में रखने की इच्छा सैद्धांतिक तौर पर मजबूत है। देश में सेमीकंडक्टर को लेकर समुचित माहौल नहीं होने के कारण बड़े पैमाने पर प्रतिभा पलायन हुआ और सिलिकन वैली के शीर्ष चिप निर्माताओं ने भारत में डिजाइन केंद्र स्थापित करके भारत की प्रतिभाओं का लाभ उठाया। सेमीकंडक्टर कारोबार में मूल्यवर्धन की बुनियाद डिजाइन है, न कि निर्माण। यही कारण है कि सिलिकन वैली की दिग्गज कंपनियां मसलन इंटेल, क्वालकॉम, एनविडिया तथा बाद में एएमडी तथा अन्य कंपनियों ने महंगी विनिर्माण प्रक्रिया में निवेश नहीं किया। इसके बजाय इन कंपनियों ने अपना पूरा ध्यान उन्नत तकनीक विकसित करने पर लगाया और सन 1970 के दशक में ही एशिया में ताइवान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान जैसी जगहें तलाश कीं ताकि एक विशालकाय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके। बौद्धिक संपदा पर ध्यान केंद्रित करके सिलिकन वैली बिना विनिर्माण प्रक्रिया पर दबदबा कायम किए इस पूरे उद्योग पर भारी असर रखती है। घरेलू चिप डिजाइन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के भारत सरकार के प्रस्ताव को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
इस योजना के साथ दिक्कत यह है कि यह इस उद्योग के गुणों की अनदेखी करती है। सेमीकंडक्टर डिजाइन उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धा वाले नवाचारी माहौल में फलता-फूलता है जो गतिशीलता पर निर्भर है। इसके अलावा इसमें लगातार नाकामियों को सहन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। ऐसा रचनात्मक माहौल तैयार करने के लिए सरकार को खुद को भी रातोरात बदलना होगा। समय खपाऊ मंजूरी प्रणाली जहां डिजाइनरों से निवेश हासिल करने के लिए अपने डिजाइन की अवधारणा पेश करने को कहा जाता हो वह इसमें मददगार न हो सकेगी।
दूसरी बात, निजी क्षेत्र के साथ काम करने का भारत सरकार का प्रदर्शन कोई खास अच्छा नहीं रहा है। बाल्को और हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियों की बात करें तो इनमें सरकार ने विनिवेश के बाद हिस्सेदारी बनाए रखी थी लेकिन ये उदाहरण चिप निर्माण के क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को लेकर बहुत भरोसा नहीं पैदा करते। अधिक रचनात्मक रुख यह होगा कि घरेलू चिप निर्माताओं को भारत और विदेशों में बाजार तैयार करने में मदद करके प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए आंशिक रूप से कारोबारी सुगमता की राह की दिक्कतों को दूर करना होगा। सिलिकन वैली तभी फली-फूली जब उसने उपभोक्ता वस्तुओं के तेजी से विकसित होते बाजार पर ध्यान दिया। व्यापक अर्थव्यवस्था में से अकेले औद्योगिक क्षेत्र के दिग्गजों को चुनने से बहुत अच्छे नतीजे नहीं हाथ लगेंगे।
कारोबार का विस्तार
संपादकीय

अब ताजा समझौते के अमल में आने का प्रत्यक्ष असर यह होगा कि भारत और यूएई में आपसी कारोबार में बढ़ोतरी के साथ-साथ लेनदेन और भुगतान में कम समय लगेगा और आयातकों-निर्यातकों को डालर का इंतजाम किए बिना भुगतान करने में सुविधा होगी। इसके अलावा, मुद्रा बाजार में रुपए और दिरहम में निवेश करने का विकल्प भी खुलेगा और पर्यटन सुविधाजनक होगा। कहा जा सकता है कि जिस दौर में अमेरिका अपनी मुद्रा डालर के प्रभाव के बूते वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव कायम रखे हुए है, उसमें भारत और यूएई के बीच अपनी अपनी स्थानीय मुद्रा में कारोबार पर बनी सहमति कूटनीति स्तर पर एक नया परिदृश्य रचेगा। दरअसल, अमेरिकी डालर के वर्चस्व की वजह से पहले से ही कुछ देशों की ओर से कारोबार के मोर्चे पर नए समीकरण खड़ा करने की कोशिश चल रही है। कुछ बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश वैश्विक स्तर पर कारोबार के ढांचे में अमेरिकी डालर का विकल्प तलाश रहे हैं। इसमें खासतौर पर रूस, चीन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। यहां तक कि बांग्लादेश जैसे छोटे एशियाई देश भी आपस में व्यापार के लिए स्थानीय मुद्रा को तरजीह दे रहे हैं।
यह छिपा नहीं है कि वैश्विक स्तर पर कारोबार जगत में कई स्तर पर उतार-चढ़ाव चल रहे हैं। एक समय डालर पर निर्भर दुनिया अब नए विकल्पों का रुख कर रही है। इसका कारण संभवत: यह हो सकता है कि हाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के अलग-अलग ध्रुव खड़े हो रहे हैं और उसी मुताबिक आर्थिक जगत में भी नया स्वरूप तैयार हो रहा है। इसमें भारत की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। रूस से तेल खरीदने के लिए भारत और यूएई दिरहम और रूबल का उपयोग कर रहे हैं। उधर चीन के भी हाल में युआन से 88 अरब डालर का रूसी तेल, कोयला और धातु खरीदने की खबर आई थी। बल्कि वैश्विक स्तर पर विदेशी मुद्रा लेनदेन में युआन की हिस्सेदारी बढ़कर सात फीसद पर पहुंच गई है। इस लिहाज से देखें तो भारत और यूएई के बीच हुआ ताजा समझौता मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस करार को पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में आई नई गरमाहट की अगली कड़ी माना जा सकता है।
नये अध्याय का प्रारंभ
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का फ्रांस में जैसा स्वागत हुआ, वह ऐतिहासिक और अभूतपूर्व था। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में भारतीय प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करने के साथ ही उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित करना द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बहुत अहम है। इससे नई दिल्ली और पेरिस के संबंधों में एक नये अध्याय की शुरुआत हुई है। रक्षा उपकरणों एवं हथियारों के उत्पादन में एक दूसरे का सहयोग, जलवायु परिवर्तन जैसे ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे के साथ खड़े रहना, और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग करना द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के मुख्य स्तंभ हैं। इस तरह भारत और फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद जिस ठोस धरातल पर रखी गई है, उससे एक अहम सवाल उठता है कि क्या भारतीय विदेश नीति का झुकाव रूस की बजाए फ्रांस की तरफ हो रहा है? रूस सोवियत संघ के जमाने से ही भारत का भरोसेमंद मित्र रहा है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उसने खुलकर भारत का समर्थन किया था। दूसरी ओर, फ्रांस के साथ भी भारत का पिछले 25 वर्षो से मधुर रिश्ता है। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण में दूसरा सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, तब भारत को दंडित करने के लिए अमेरिका ने सख्त प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का सदस्य होने के बावजूद फ्रांस ने इसकी मुखालफत की थी। इसी तरह, 2019 में कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के सवाल पर सुरक्षा परिषद में उसने भारत का साथ दिया था। हालांकि रूस के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों के संबंधों में कुछ खरोचें आई हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस युद्ध में भारत के तटस्थ रुख से नाखुश हैं। अमेरिका की रूस विरोधी नीतियों ने मास्को और बीजिंग को एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया है, लेकिन पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी अतिक्रमण को रोकने की दिशा में रूस से भारत को मायूसी मिली है। इसी बीच, भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है, लेकिन वहां के थिंक टैंक, मीडिया और प्रबुद्ध वर्ग मोदी की कथित अल्पसंख्यक विरोधी नीति और मानवाधिकारों के सवालों को लेकर उनकी आलोचना करता रहता है, जिससे भारत अमेरिका के प्रति हमेशा सशंकित रहता है। लेकिन फ्रांस ऐसा यूरोपीय देश है, जिसके साथ भारत बहुत सहज महसूस करता है।
Date:18-07-23
कृषि क्षेत्र में मुकाबला
संपादकीय
जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्र में उत्पादन व उत्पादकता को सतत बनाए रखने की एक गंभीर चुनौती है। यह केवल भारत जैसे कृषि प्रधान देश तक सीमित नहीं है-पूरे विश्व तक फैली है। इससे पुराने तौर-तरीकों से नहीं निबटा जा सकता। इन बदलावों को सहन करने वाले खाद्यान्नों की नई किस्म विकसित करनी होगी और उनकी सिंचाई के नियमित संसाधनों पर विशेष ध्यान देना होगा। यह अच्छी बात है कि सरकार भी इस पर गंभीरतापूर्वक सोच रही है। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर कहते हैं कि इसके अनुरूप फसलों की नयी-नयी किस्में विकसित की गई हैं। कृषि अनुसंधान परिषद के 95वें स्थापना व प्रौद्योगिकी दिवस पर उन्होंने कहा कि इसके लिए मृदा की उर्वरकता पर ध्यान देना होगा, जो रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से नष्ट हो गई है और वैकल्पिक जैविक व प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना होगा। यह तरीका जलवायु-बदलावों का बेहतर सामना कर सकता है। जैविक व प्राकृतिक उत्पाद बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं पर वे इतने महंगे हैं कि आमजन की थाली में नहीं आ सकते। ऐसा इन खाद्य पदार्थों की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण न होने के चलते है। परंतु सरकार इस खेती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा दे तो उनके पुष्टिकारक उत्पादों तक सबकी पहुंच हो सकती है। इसके साथ, खेती-किसानी की मूल समस्या बढ़ती लागत और पैदावारों के उचित मूल्य न मिलने पर भी ध्यान देना होगा। बाढ़, सूखा, पाला गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी खेती को महफूज रखने के ठोस इंतजामात को भी जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में शामिल करना चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए कि दुनिया के खान-पान विशेषज्ञ भारतीय भोजन की थाली को विविधतापूर्ण, स्वादिष्ट एवं सेहतमंद मानते हैं। इसी वजह से 2022 के बेस्ट ग्लोबल कुजिन्स की सूची में भारतीय व्यंजनों को पांचवीं श्रेणी मिली है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ हमारी थाली को उतना पोषण-क्षम नहीं मानते। मगर जैसा कि कृषि मंत्री ने कहा यदि हम इन आवश्यकताओं को समझते हुए उत्पादन व उत्पादकता को बेहतर करने के प्रयास करते हैं तो जल्द ही हमारी भोजन की थाली पोषण से भरपूर हो सकेगी। साथ ही, कृषकों-उपभोक्ताओं को उचित मूल्य में चीजें मुहैया कराने के सरकारी प्रयासों को उचित धरातल मिल सकती है। नित नये व वैज्ञानिक प्रयोगों व प्रयासों से होने वाले परिवर्तन तमाम चुनौतियों से जूझने की राह प्रशस्त कर सकेंगे।
Date:18-07-23
ऐतिहासिक दौर में साझेदारी
अवधेश कुमार
फ्रांस की राजधानी पेरिस में राष्ट्रीय दिवस समारोह बस्ताइल दिवस परेड में फ्रांसीसी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के तीनों अंगों के 241 सदस्यीय मार्चिंग दस्ते को परेड करते, सैनिक बैंड द्वारा सारे जहां से अच्छा धुन बजाते सुन तथा राफेल विमानों का परेड के दौरान फ्लाईपास्ट का हिस्सा बनता देख समूचे भारत ने गर्व का अनुभव किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। मैक्रों ने ट्वीट में लिखा विश्व इतिहास में व भविष्य में निर्णायक भूमिका निभाने वाला एक रणनीतिक साझेदार, एक मित्र। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया कि अपने सदियों पुराने लोकाचार से प्रेरित भारत विश्व को शांतिपूर्ण समृद्धि और टिकाऊ बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एक मजबूत और भरोसेमंद भागीदार होने के लिए 1.4 अरब भारतीय हमेशा फ्रांस के आभारी रहेंगे। सन् 2009 में भी फ्रांस ने नेशनल डे परेड में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया था। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस या बस्ताइल दिवस इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह 1789 की प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बस्ताइल जेल पर हमला कर कैदियों को मुक्ति कराने का दिवस है। वहीं से फ्रांस में परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। आधुनिक विश्व में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति से ही निकला है। फ्रांस ने अपना सबसे बड़ा नागरिक और सैन्य सम्मान द ग्रैंड क्लास ऑफ ‘द लीजन ऑफ ऑनर’ प्रधानमंत्री मोदी को दिया। मैक्रों ने लूव्र संग्रहालय में मोदी को दावत दिया।
फ्रांस ने 70 वर्ष में पहली बार किसी विदेशी नेता के सम्मान में लुव्र के बैंकट हॉल को खोला। 1953 में यहां ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में भोज दिया गया था। यहां राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री को एक उपहार दिया जिसमें 1916 में ली गई तस्वीर की प्रति है। इसमें एक व्यक्ति इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स आईएएफ अधिकारी को फूल भेंट कर रहा है। यह तस्वीर उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने 1914-1918 में फ्रांस के साथ यूरोप में लड़ाई लड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बताया कि जिस रेजीमेंट के जवानों ने तब फ्रांस की रक्षा के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया उसके पंजाब रेजीमेंट के जवान परेड में हिस्सा ले रहे हैं। मोदी और मैक्रों की द्विपक्षीय वार्ता की अनोखी बात यह रही कि दोनों नेताओं ने परंपरा से अलग बैठक से पहले प्रेस के सामने बयान जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम रक्षा क्षेत्र में भारत में नई प्रौद्योगिकी के सह विकास पर बात कर रहे हैं। वास्तव में रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच संबंधों का एक आधारस्तंभ है। भारत विभिन्न देशों के साथ सामरिक साझेदारी बढ़ाने के साथ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने पर फोकस कर रहा है। इसमें फ्रांस इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वह अत्याधुनिक रक्षा उपकरण भारत को देना चाहता है। तकनीक साझा कर भारत में उनके उत्पादन को प्रोत्साहन देने में भी उसे समस्या नहीं है। मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत में फ्रांस रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा साझीदार बन रहा है।
यह तय हुआ कि पनडुब्बी से लेकर नौसेना के विमान आदि अपने साथ मित्र राष्ट्रों की आवश्यकताओं के हिसाब से निर्मिंत किया जाए। हम अमेरिका या रूस आदि के साथ भारत में उत्पादन या दोनों देशों का ध्यान रखते हुए उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण की सीमा तक बढ़े थे। भारत ने फ्रांस से राफेल के 26 नौसेना संस्करण राफेल-एम के साथ तीन और स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की खरीद का सौदा किया है। नौसेना के लिए तैयार यह राफेल अनेक विशिष्टता रखता है। फ्रांस स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की तकनीक भी हस्तांतरित करेगा। इससे इनका निर्माण भारत में होगा। पांचवीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान और मल्टीरोल हेलीकॉप्टरों के इंजनों के लिए बातचीत अंतिम चरण में है। दोनों देश नाभिकीय ऊर्जा के लिए छोटे व अत्याधुनिक रिएक्टर बनाने में भी सहयोग करेंगे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर विश्व के प्रमुख देशों का फोकस है। भारत-फ्रांस ने हिंद-प्रशांत को लेकर रोडमैप जारी किया, जिसके मुताबिक दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के साथ अपनी सेना की मौजूदगी और संपर्क बढ़ाएंगे।
फ्रांस जहां भारत में रक्षा औद्योगिक क्षमताओं के विकास में मदद करेगा, वहीं भारत लारी यूनियन, न्यू केलेडोनिया और फ्रेंच पोलिनेशिया जैसी फ्रांसीसी बस्तियों की सुरक्षा में मदद करेगा। इन बस्तियों में फ्रांस के करीब 15 लाख लोग और आठ हजार से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। भारत नौसेना के 26 राफेल का इस्तेमाल हिंद-प्रशांत में अपनी स्थिति को मजबूत करने में करेगा। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में फ्रांस प्रभावी मौजूदगी नहीं है। दोनों देश अपने हितों को देखते हुए अलग-अलग मंचों पर साझेदारी भी बढ़ा रहे हैं। फ्रांस ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर एक मोर्चा मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत के लोग खुद को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प कर चुके हैं।
नरेन्द्र मोदी की यात्रा फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के साथ भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरा होने के अवसर से भी जुड़ा था। 1998 में नाभिकीय विस्फोट के बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था, पर फ्रांस ने भारत का समर्थन किया और उसी समय उसने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की। फ्रांस ने पश्चिमी देशों के उलट जाकर भारत को नाभिकीय प्लांट लगाने में मदद की। इस नाते फ्रांस और भारत के संबंधों का महत्त्व समझ में आता है। भारत और फ्रांस के बीच अनेक वैश्विक मुद्दों पर सहमति है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार फ्रांस भी चाहता है और उसने भारत की स्थायी सदस्यता का पक्ष लिया है। दोनों देश बहुपक्षीय विश्व के समर्थक हैं। इस्लामी आतंकवाद के विरु द्ध लड़ाई में भी दोनों की सोच मिलती है। हमारे राष्ट्रीय हित उनके साथ मेल खाते हैं, स्वयं को प्रभावी वैश्विक शक्ति यानी महाशक्ति बनने के हमारे लक्ष्य से वह सहमत दिखता है तथा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वर्तमान भारतीय नेतृत्व की कल्पना के अनुरूप अगर फ्रांस की दृष्टि है तो मोदी मैक्रों के बीच का आपसी विश्वास के बीच साझेदारी सशक्त होती जाएगी।
चीतों की चिंता
संपादकीय
भारतीय जंगलों में चीता को फिर बसाने का अभियान जितना कठिन है, उतना ही आवश्यक भी है। यह पशुओं के प्रति निरंतर संवेदनशील होते एक राष्ट्र की ओर से किया जा रहा भूल सुधार का प्रयास भी है। जहां एक ओर एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जो इस प्रयास को अब दुखद मानते हैं, वहीं जो लोग इस प्रयास को सुखद बनाने में जुटे हैं, उनकी मेहनत पर भी सबको गौर करना चाहिए। 17 सितंबर, 2022 को चीते भारत लाए गए थे और उसके बाद से आठ चीतों की मौत हो चुकी है। जान गंवाने वाले चीतों में पांच बडे़ चीते थे, जो आयात किए गए थे और तीन शिशु थे, जो यहीं कुनो, भारत में जन्मे थे। आठवें चीते की मौत के बाद कुछ ज्यादा आलोचना हुई, तो अब सरकार की ओर से सफाई आई है कि चीतों की मौत का कारण उनकी गर्दन पर बंधा रेडियो कॉलर से हुआ संक्रमण नहीं है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने कहा है कि सभी मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने अफ्रीका के अनुभवों का भी हवाला दिया है, वहां भी पहले चीतों को बसाने की कोशिश में शुरुआती चरण में 50 प्रतिशत मौतें देखी गई थीं।
चीता अभियान को संभाल रही सर्वोच्च संस्था, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को पूरा भरोसा है कि भारत में फिर चीतों को बसाने का अभियान सफल होगा। अभी अभियान को शुरू हुए साल भर भी नहीं बीता है, तो अभी से इस अभियान को नाकाम करार देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीतों को लेकर कई अफवाहों और अटकलों का आलम है। कई नस्ल के चीते एक समय भारत में मौजूद थे, अत: यह कहना सही नहीं है कि भारत में चीतों के अनुकूल माहौल नहीं है। हां, चीते स्वभाव से नाजुक या संवेदनशील होते हैं और उन्हें अपने मूल देश या परिवेश का अभाव महसूस हो सकता है, पर यह भी तथ्य है कि अभी भी 11 चीते आठ-दस महीने से भारतीय जंगलों में खुले में रह रहे हैं। पांच चीतों को, जिनमें एक शिशु भी शामिल है, क्वारंटीन में रखा गया है। चीता संरक्षण से जुड़े लोगों का मानना है कि यह एक दीर्घकालिक योजना है, अत: इंतजार करना चाहिए। इसमें शक नहीं कि चीतों को प्राकृतिक रूप से बचाने की कोशिश हो रही है। उन्हें किसी बाडे़ में रखकर दिन-रात की देखभाल से बचाने की कोशिश भी हो सकती है, जैसा कुछ के साथ किया जा रहा है, लेकिन अभियान की सफलता तभी है, जब कुनो में चीते स्वाभाविक रूप से वंशवृद्धि करने लगें।
भारतीय विशेषज्ञ लगातार अंतरराष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के पशु चिकित्सकों के साथ संपर्क में हैं। चीता पोषण की तमाम सावधानियों को आजमाया जा रहा है। किसी को दोष देना आज के समय में आसान काम है, लेकिन जरूरत समझदारी की है। इस देश में 70 साल पहले हजारों चीतों को बेरहमी से मारकर खत्म कर दिया गया, काश! हम तब संवेदनशील रहे होते। अच्छी बात है कि हमारी संवेदना आज जागी है, आज हमारे लिए एक-एक चीता जीवन मूल्यवान हो गया है। भारत सरकार ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ निकट समन्वय में काम करने के लिए एक समर्पित एनटीसीए टीम तैनात की है। हमें विशेषज्ञों पर भरोसा रखना चाहिए और विशेषज्ञों को भी देश के इस महत्वाकांक्षी अभियान को पूरी पारदर्शिता के साथ सफल बनाते हुए अपनी योग्यता सिद्ध करनी चाहिए।