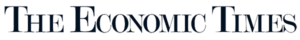18-06-2016 (Important News Clippings)
Date: 17-06-16
Rebuilding The University
It calls for clear, original thinking from policymakers and stakeholders
Thousands of professors have taken to the streets, putting aside their ideological differences, to protest against the bizarre service guidelines laid down in the UGC (University Grants Commission) Gazette Notification of 2016, the third amendment in only six years. The main issues concern their workload and promotions. While the workload issue seems to have been resolved in the recent full commission meeting of the UGC, the official notification is still awaited.
Promotions in universities are now made on the basis of a performance-based appraisal system (PBAS) wherein the tasks of professors are broken down into quantifiable indicators and points are assigned for each. There are three broad categories under which one is assessed: One, teaching, learning, and evaluation; two, co-curricular activities; and three, research. While there are some advantages to this system, it has been poorly thought out in that the emphasis is on quantity and not quality.
One also needs to look at the timeline of these amendments. The first set of promotion guidelines was issued by the UGC in 2010 and, defying all logic, was made effective retrospectively from 2008. The professors who became eligible for promotion between 2008-10 and whose interviews were held in time during this period got promoted under the old Merit Promotion Scheme, but those whose interviews got delayed beyond 2010 (and this is quite common in government organisations) will now be required to apply under the new, significantly stricter PBAS. This raises two questions: One, how can candidates who qualify for promotion at the same time be subject to two different sets of rules? Two, how can any reasonable government expect a candidate to change his portfolio based on its whimsical fancies? The latest amendment has only created further uncertainty as it changes the rules of the game yet again.
Clearly, policymakers lack an understanding of the profession. Every aspect of a teacher’s job is not contractible. The care and attention a teacher gives is not quantifiable but matters a great deal in how we nurture young minds. When some aspects of performance are not measurable, the employee is bound to shift his attention away from these tasks to those that can be measured and rewarded. Also, note that earning points greater than the required minimum does not translate into a higher salary!
Our goal is to build strong and internationally competitive institutions of higher education. But we don’t even have the basic infrastructure to support teaching and research. Undergraduate professors sit in a common staff-room and have no designated office space that is available even to a graduate student in the West. Having a teaching or research assistant, which is a given in high ranking universities, is something one can’t even dream about here. Research grants are almost always released years after a project is completed. Can world-class research (or any class of research) be expected in this scenario?
The nature of a job at the undergraduate level, at least in Delhi University, is more teaching driven and very different from that at the postgraduate level. In particular, the emphasis is more on categories like teaching, learning, and evaluation than research. In the US, there is a clear distinction between a teaching position and a research position. In all this, good teaching is being compromised.
Higher education needs clear, original thinking on the part of policymakers and involvement of stakeholders, budgetary issues and GATS considerations notwithstanding. We must strengthen our well-established institutions of higher learning by providing at least a basic research environment. Promotions can be based on both objective and subjective criteria without solely playing “points”. Strong and healthy institutions must be in place to retain our good faculty and encourage new talent into the profession.
Date: 17-06-16
Mistrust in Manipur
There is a lingering apprehension among the hill people that the state government would use the bills as a strategic political ploy to gain control over their land.
Written by Nehginpao Kipgen
Last fortnight, Union Home Minister Rajnath Singh explained to a delegation from Manipur led by the state Chief Minister Okram Ibobi Singh why President Pranab Mukherjee returned three bills the Manipur Assembly had passed on August 31, 2015. The contentious bills were the Manipur Land Reforms and Land Revenue (7th Amendment) Bill, 2015, the Manipur Shops and Establishment (2nd Amendment) Bill, 2015, and the Manipur Protection of Peoples Bill, 2015. Experts will now re-examine the first two bills for a “reasonable conclusion” and in the case of the third bill, legal and constitutional experts will re-examine it for a “new legislation taking into consideration all aspects of the hill and valley people of Manipur.” The question now is what steps should be taken to bring a mutually acceptable agreement.
The British colonial government had introduced the Inner Line Permit (ILP) to protect its commercial interests. Later, it was used as an instrument to protect the tribal people and their cultures. Since Manipur is not officially a tribal state, there are constitutional challenges to implementing the ILP system. Had the Manipur Protection of Peoples, 2015 bill become law and got implemented strictly, many of the hill people (the Kukis and the Nagas) could have found themselves declared non-Manipuris since the bill requires a person to have been enumerated in all three registers — the National Register of Citizens, 1951, the Census Report 1951, and the Village Directory of 1951. In 1951, most of the hill areas were not accessible by road and the situation remains the same in some places even today.
There is a lingering apprehension among the hill people that the state government would use the bills as a strategic political ploy to gain control over their land. The unwillingness on the part of the state government to implement the Sixth Schedule in the hill areas has exacerbated the concerns of the tribal people. Had the bills been enacted into law, they will be applicable across the state of Manipur, including the hill areas. But the drafting committee formed by the state government did not involve tribal legislators. People of the hill areas were not consulted in the process of drafting the bills.
The valley people (the Meiteis, who dominate state government) argue that the bills are largely misunderstood and misinterpreted by the hill people. They claim that the bills are not detrimental to the interests of the hill people. But the irony is neither the government nor the Meiteis took steps to convince the tribal people, or the Joint
Action Committee Against Anti-Tribal Bills (JACAATB), the body spearheading the agitation.
On December 29, 2015, Chief Minister Ibobi Singh met an 18-member delegation of the JACAATB, which requested the CM to convene a special session of the Manipur Legislative Assembly to review the concerns and apprehensions of the hill people. Singh then requested the delegation to list their concerns regarding the three bills in writing. Subsequently, on January 11 this year, the
JACAATB submitted a six-page document outlining what they thought was “anti-tribal” and infringement on the constitutionally guaranteed tribal rights in the bills. Since then, there has been no substantial talk between the two sides.
The classification of the Protection of Manipur People Bill, 2015 as a money bill was sinister, as it was done to bypass the Hill Areas Committee. The expenditure from the consolidated fund is only incidental and not the main provision of the bill. The Manipur Legislative Assembly (Hill Areas Committee) Order, 1972, states that “every bill, other than a money bill, affecting wholly or partly the hill areas and containing mainly provisions dealing with any of the scheduled matters shall, after introduction in the Assembly, be referred to the Hill Areas Committee for consideration and report to the Assembly.”
Given the deep division between the hill and valley people on the issue, it was a right decision on the part of the president to return the bills back for re-examination by legal and constitutional experts. The state government should now take steps to build trust between peoples of the hill and the valley, as well as the hill people and the state government. The government should take steps to initiate a dialogue between the representatives of the Joint Committee on Inner Line Permit System and the JACAATB. Meanwhile, the state government should act against police personnel responsible for the death of nine tribal people, whose bodies remain unburied for more than 250 days.
The recent pattern of violence in the state has the potential of not only dividing the people but also a danger of territorial disintegration if left unaddressed.
Date: 17-06-16
Weakening the watchdog
- M. R. MADHAVAN
The Delhi government has appointed 21 MLAs as parliamentary secretaries. Several other State governments have also taken this route in the past; earlier State governments in Delhi have also made such appointments, although fewer in number. This is part of a trend of weakening the power of legislative bodies by governments which has developed over the last three decades.
Most modern republics build in the concept of separation of powers in their Constitutions. The idea is that no particular organ of state should have a concentration of powers. Different institutions act as a check on the actions of others. In the simplest form, there are at least three parts: the executive arm that makes and executes policies, the legislative arm that makes laws and holds the executive to account, and the judicial arm that adjudicates disputes and ensures that the other two arms do not violate the provisions of the Constitution. In particular, Parliament and State legislatures have the important duty of monitoring the actions of the government and holding it to account. Our Supreme Court has recognised separation of powers as part of the basic structure of the Constitution, and can therefore strike down even amendments to the Constitution that infringe upon this principle.
Checks and balances
The concept of office of profit finds place in Articles 102 and 191 of the Constitution, which state that an MP or MLA will be disqualified if he or she occupies such an office. The idea is that every legislator should be able to carry out legislative duties without any obligation to the government of the day. As Ministers have to be members of the legislature, they are exempt from this disqualification. The Constitution also recognises that there may be other cases where exceptions may be required and allows Parliament and State legislatures to make exemptions by passing a law. In several cases, courts have examined this issue and concluded that the key question is whether occupation of such office will make a legislator beholden to the executive. In general, a person is considered to hold an office of profit if four conditions are met: (a) he holds an office, (b) the office is one of profit, that is, it carries some benefits, (c) the office is under the control of the Central or the State government (d) the office is not that of a Minister or exempted by an Act of Parliament or State legislature.
The 91st amendment to the Constitution recognised the problem of the government trying to win over legislators by giving them ministerial berths. It limited the number of ministers, including the Chief Minister, to 15 per cent of the strength of the Lok Sabha or State Legislative Assemblies. For Delhi, Article 239AA of the Constitution limits the number to 10 per cent of the strength of the Legislative Assembly (which is seven persons). The question is whether by appointing 21 more MLAs as parliamentary secretaries — which will make 40 per cent of the membership have some type of an executive role — the nature of the Legislative Assembly is being changed. That is, whether such an Assembly will still be able to exercise its oversight role over the government. An argument has been made that these parliamentary secretaries will be able to aid the government in being more responsive to citizens’ needs. That argument, however, misses the point of separation of powers. The role of legislators is not to help the government do its job better, but to ensure that it functions in a proper manner. That is, the legislator exercises the role of a watchdog over the government on behalf of citizens and not as an agent of the government.
Disempowering the legislature
Two other developments, the anti-defection law and MPLADS/MLALADS (local area development schemes), also weaken the separation of the legislative arm from the executive. The anti-defection law was enacted in 1985 through the 52nd amendment to the Constitution. This requires all legislators to abide by the party diktat on every vote in the legislature. Therefore, the legislator cannot exercise independent judgement on any issue if the party leadership has taken a position. Thirty years of experience shows us that this has led to concentration of power in party leaderships. For instance, one sees any government that is trying to build consensus — such as for the Goods and Services Tax legislation — negotiate with the leaderships of various parties, rather than convince individual MPs on the merits of the case. Also, the ruling party can require all its MPs to vote in support of a motion. These MPs have effectively lost their rights — and therefore cannot do their duty — of exercising their independent judgement on issues and performing the watchdog role.
In 1993, the Central government started MPLADS, through which legislators can earmark a certain amount of public funds for projects in their constituency. The concept has been adopted by many states as MLALADS. The argument was that elected MPs and MLAs know the needs of their electorate well and can be effective in allocation of resources. This again subverts the role of legislators. Their role is to allocate the entire Central and State budgets, and to monitor the spending. They are expected to use their knowledge of ground-level issues in this allocation, and see that the funds are spent properly. By providing each of them a specific amount to spend on projects, their oversight role is weakened.
The role of legislators is critical in a democracy. They are elected by citizens, and have the task of ensuring that the government is acting in the best interests of the public. In this, they are expected to exercise their independent judgements on what constitutes public and national interest. They act as a bulwark against autocratic actions of the executive. Therefore, it is imperative that their independence is protected. Actions that impinge on such independence, such as excessive appointments to executive positions, the anti-defection law and MPLADS, should be reversed. Otherwise, there is a risk of a slow erosion of the institution of legislatures, which could put at risk the very existence of our republic.
M.R. Madhavan is the President and co-founder of PRS Legislative Research.
Date: 17-06-16
Views to watch
There is little that is surprising about India’s recent refusal to allow Google to launch its Street View service, which gives users a 360-degree view of public spaces. As this newspaper has reported, the proposal was rejected following objections raised by the Defence Ministry. The decision is said to have come in the backdrop of the terror attack on the Pathankot airbase in January, with investigators suspecting that terrorists used Google Maps to study the topography of the targeted area. Barely days after the airbase attack, the Delhi High Court asked the government to examine the issue of sensitive locations such as defence installations and nuclear power plants showing on Google Maps. It isn’t clear if these concerns have been addressed. Street View goes a step further than the maps. It displays panoramic views of public spaces, thanks to images captured by Google’s moving vehicles, adding a layer of depth and reality to the maps. India has hinted that its refusal is not final and that such issues could be resolved once the Geospatial Bill, which seeks to regulate map-creation and sharing, comes into force. But it is unclear whether this will help, given that the proposed legislation is somewhat overenthusiastic about regulation. India isn’t the first country to seem troubled by Street View. Since its launch in 2007 in the U.S., the service has faced roadblocks in many countries. In the U.S., for instance, both the Department of Homeland Security and the Department of Defense had concerns over Google capturing images of sensitive locations. In Europe, especially Germany, concerns over loss of privacy took centre stage. The script wasn’t different in Japan.
And yet, Street View is available in all these countries. Solutions were eventually found. Before long, the service figured out a way to blur people’s faces and licence plates automatically before the pictures were made public. In the U.S., Google was asked to remove sensitive information, and its image-capturing cars were ordered to keep off military bases. In Germany, households were given the option of blurring their buildings. In Japan, the height from which the cameras scanned the neighbourhoods was lowered and local governments were notified prior to Google’s photography. Even Israel, which takes internal security very seriously, gave the green signal to Street View five years ago, reportedly making sure Google doesn’t show images in real-time and only photographs public spaces open to all. While there is an obvious tourism angle involved, Google representatives have spoken of Street View’s usefulness in disaster management. All things considered, it might not be in India’s best interests to keep out this technology for long.
Date: 18-06-16
Adequate storage for hybrid renewables
There is much potential for solar plants and wind farms to be complementary as the latter can function while the former is inactive. It follows that solar-wind hybrid systems can reduce variability in generation and bring about better grid integration. But the draft national wind-solar hybrid policy seems to put the cart before the horse, as it were.
The draft policy says the central regulatory commission should firm up guidelines for determining tariffs for the hybrid systems, and further that the body needs to frame guidelines for scheduling and wheeling power from the hybrids. But in the absence of such critical norms, to expect investments to actualise suggests the triumph of hope over experience. The draft text is replete with trite truisms: there is scope for solar photovoltaic capacity in existing wind farms, and wind potential in the vicinity of solar plants. The policy avers that the hybrid power fed into the grid will not be more than the transmission capacity/grid connectivity allowed for existing wind or solar project. But it is obvious that adequate line capacity is required for evacuation. Storage is another vital challenge.
The policy does rightly mention that solar and wind power being infirm in nature pose challenges for grid security and stability. And as we aim to scale up solar- and wind-operated power plants to utility size, we need to be seized of the issues of grid stability and power storage for renewable energy plants. The policy does mention in the fag end that the government would support development of standards and technology for hybrid systems. But there seems much too much focus on garnering fiscal, financial and various other incentives for individual stand-alone solar and wind projects. Such a policy stance can plain mis-allocate resources and lead to high costs.
Date: 18-06-16
Smoothen Out Distortions
Market-friendly or simply business-friendly? It depends on how India pushes for real reformsThe Narendra Modi government swept into power two years ago on a reform agenda. The prime minister had promised to unlock the latent power of the private sector to drive increased economic activity and initiated a reform process that has proved difficult to fully realise.
National-level reform is difficult everywhere. But it seems particularly so in India. Evidence from the transitions in the former Soviet Union and Latin America, in particular, shows that opening trade and border barriers, without addressing internal economic distortions — government restraints that are anti-competitive — also often leads to partial reform and crony capitalism.
It has proved difficult to overcome the vested interests that benefit from these distortions, or anti-competitive market distortions (ACMDs). In this regard, India’s experience is not so different from the experience in other markets that are also in the process of reform.
ACMDs are typically laws or regulations that protect a privileged or vested-interest elite group by blocking competition or artificially raising the costs of competitors. India has adopted a form of these with its embrace of local content regulation in a number of areas.
Simply being business-friendly is not enough. For true reform, government policies must be market-friendly. A host of protective regulation shelters under the guise of being business-friendly (usually protecting preferred, privileged businesses).
On May 23, the Legatum Institute, a global think tank based in London, launched a ground-breaking report on the challenges and opportunities faced by the modern Indian economy. ‘Anti-Competitive Market Distortions and Their Impact: A Case Study of India’ (goo.gl/jOwJxs) explores potential growth areas for the country and quantifies the cost of inaction across several key sectors through the focal lens of domestic competition, trade and property rights.
Garibi Hatao, Here’s How
The study’s results are dramatic:
If India eliminated all its distortions, it would be the fifth-largest economy in the world, and in GDP per-capita terms, it would rise from being ranked 169th to being ranked 67th.
If India eliminated all its distortions, it would generate over 200 million new jobs, and reduce absolute poverty to zero.
If India improved its insolvency rules, opened up to foreign investment in certain areas and better protected intellectual property rules, the number of people living on less than $2 per day would be reduced from 770 million to 627 million.
Simply optimising its regulatory environment with regard to the World Bank’s ‘Doing Business Index’ would lead to a productivity gain of only 0.07%. This is because deeply embedded structural issues hamper India’s economic development. Simply improving business registration processes and procedures will lead to some new business creation, but will not be sustainable unless accompanied by deeper reforms.
Improving its insolvency rules, opening up to foreign investment in certain areas and better protecting intellectual property (L2) could lead to a productivity gain of 148%.
Removal of distortions across the dimensions of trade, competition and property rights protection could lead to a GDP gain of around 650%.
Labour market flexibility is a key driver and accounts for about a quarter of the overall GDP gain possible.
The report additionally contains a treatment of both the civil aviation (goo.gl/5bs6KE) and the cotton-textile-garment sector (goo.gl/byF0hD) where there are significant distortions. This is particularly impactful in India where so many people are employed in these sectors.
The opportunity for India to completely eliminate poverty is, by far, the most outstanding finding of this report, and the most encouraging to the future of the country. At present, nearly 60% of Indians (770 million people) live on $2 a day or less, and roughly 23% of Indians (307 million people) live on $1.25 a day or less.
The second level of the report’s modelling posits removal of many ACMDs, including the allowance of foreign currency bank accounts, removal of international capital controls, improving insolvency provisions, shoring up intellectual property protection and increasing transparency of government policymaking.
Implementing these changes would result in an 11% reduction in the number of Indians living on less than $2 a day (143 million people lifted out of poverty), and a 4.5% reduction in the number of Indians living on less than $1.25 a day (59 million lifted out of poverty). The total elimination of distortions in India is, of course, impossible. But this represents an aspirational goal. The 656% increase in GDP would lead to the complete elimination of poverty at $2 a day and $1.25 a day in India.
Dear Darlin’, You’re Fired
If the Indian people are to reap the rewards that can be gained from a reduction of distortions, the government will need to seize the initiative and push structural reform even in the teeth of resistance from the beneficiaries of distortions.
The test for the Indian government is whether it is market-friendly or simply business-friendly, and whether the difference is truly understood. The stakes for the Indian economy, the Indian people and the relief of poverty could not be higher.
Singham is CEO, and Kiniry is managing associate, the Competere Group
Date: 17-06-16
डर और कर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर अधिकारियों को सलाह दी है कि वे आम लोगों के दिमाग से आयकर विभाग द्वारा सताए जाने का डर दूर करें। हमारे देश में समस्या यह है कि जनता से टैक्स वसूलने वाली ज्यादातर सरकारी संस्थाओं की छवि पुलिस जैसी है। यह माना जाता है कि ये विभाग और उनके अधिकारी-कर्मचारी जबर्दस्ती उगाही करने वाले लोग हैं, इसलिए जहां तक हो सके, उनसे दूर रहना ही अच्छा है।
भारत में कम लोगों द्वारा टैक्स देने की एक बड़ी वजह यह भी है कि लोग इन विभागों और संस्थाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, और इनसे दूर रहने में ही भलाई समझते हैं। सिर्फ आयकर ही नहीं, टैक्स वसूलने वाले तमाम विभागों का रवैया अगर दोस्ताना हो गया, तो हो सकता है कि ज्यादा बड़ी तादाद में लोग खुद टैक्स चुकाने के लिए आगे आएं। ऐसा न होने से सरकार की आय भी कम होती है और ऐसे विभाग भ्रष्टाचार के जाल में भी फंस जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर अमल होता है, तो यह स्थिति काफी हद तक बदल सकती है।
भारत में 5.43 करोड़ लोग आयकर देते हैं, जो कि भारत की कुल आबादी का सिर्फ चार प्रतिशत है। इससे यह निष्कर्ष तो नहीं निकाला जा सकता कि भारत में सिर्फ इतने ही लोगों की आय इतनी है कि वे आयकर चुकाएं। इसका अर्थ यह है कि देश में जिन लोगों को आयकर चुकाना चाहिए, उनमें से ज्यादातर यह कर नहीं चुकाते। किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष करों का योगदान अप्रत्यक्ष करों से ज्यादा होना चाहिए। प्रत्यक्ष कर किसी की आमदनी पर लगता है और इसे आमदनी के मुताबिक तय किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर चीजों पर लगते हैं और उनका बोझ हर किसी को उठाना पड़ता है, भले ही उसकी आय जो भी हो। साथ ही इसका अर्थव्यवस्था और विकास पर विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि इससे वस्तुएं और सेवाएं महंंगी हो जाती हैं। भारत में सरकारें प्रत्यक्ष कर का दायरा बढ़ाने की बजाय अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अप्रत्यक्ष करों का बोझ बढ़ाने का सीधा-सरल रास्ता अपनाती रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की आमदनी, करों के दायरे से बाहर है और इससे काले धन व भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है।
प्रधानमंत्री ने आयकर विभाग के सामने आयकरदाताओं की संख्या दस करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को अगर पाना है, तो भारत में आयकर वसूलने के समूचे तंत्र में बहुत बडे़ बदलाव करने पड़ेंगे। ये बदलाव वक्त की जरूरत हैं, क्योंकि सिर्फ चार प्रतिशत आयकरदाताओं के रहते भारत का एक आधुनिक और तेजी से लगातार विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनना मुश्किल है। इसके लिए लोगों के मन से आयकर विभाग का डर निकालना सबसे जरूरी है और साथ ही आयकर चुकाने की प्रक्रियाओं को भी सरल बनाना होगा।
कई जानकार यह सुझाव दे चुके हैं कि आयकर विभाग को कानून लागू करने वाले विभाग की बजाय सेवा क्षेत्र के विभाग की तरह बनाया जाना चाहिए। लेकिन जब सरकार के सेवा क्षेत्र के विभागों का आचरण भी पुलिसिया हो, तो आयकर विभाग के स्वरूप को बदलने से क्या होगा? हालांकि यह काम असंभव नहीं है। पिछले कुछ समय में आयकर विभाग के तौर-तरीकों में काफी सुधार हुआ है। नई सूचना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिये उसका कामकाज बेहतर हुआ है। इस बीच कई स्वागतयोग्य बदलाव भी देखने में आए हैं। अगर मंत्रालय और मुख्यालय से लेकर स्थानीय दफ्तर तक बदलाव वैसे ही हुए, जैसी उम्मीद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होगा।
Date: 17-06-16
नई उड़ान
लंबी प्रतीक्षा के बाद बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस विमानन नीति पर मुहर लगाई उसके पीछे दो खास मकसद साफ दिखते हैं। एक, घरेलू विमान यात्रा का दायरा बढ़ाना। दूसरा, उसे सस्ता और सुगम बनाना। देश में अभी लगभग सालाना आठ करोड़ हवाई टिकट बिकते हैं। नई नीति का लक्ष्य इसे 2022 तक तीस करोड़ तक ले जाने का है। इसमें दो राय नहीं कि नई विमानन नीति से देश में हवाई सफर बढ़ेगा, पर यह कहना अभी अति उत्साह होगा कि इस कारोबार की वैश्विक सूची में भारत छह साल में ही नौवें से तीसरे स्थान पर आ जाएगा। क्षेत्रीय हवाई सफर को आकर्षक बनाने के मकसद से सरकार ने आधे घंटे के किराए के लिए बारह सौ पचास रुपए और एक घंटे के लिए ढाई हजार रुपए की सीमा तय की है। पर यह प्रावधान दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के बीच हवाई सफर की सूरत में ही लागू होगा। देश में पच्चीस शहरों के बीच फिलहाल अठारह ऐसे नियमित मार्ग हैं जहां हवाई सफर का समय एक घंटे से कम है। एक घंटे तक के सस्ते किराए का मकसद देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना और इसका लाभ उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करना है। विमानन कारोबार में तेजी लाने के लिए नई नीति में कुछ और भी तजवीज की गई है। जैसे, 5/20 का नियम खत्म कर दिया है। इस नियम के तहत उन्हीं विमानन कंपनियों को विदेशी उड़ानों की इजाजत दी जाती रही है जिनके पास पांच साल का अनुभव और कम से कम बीस विमान हों। अब विदेशी उड़ान की शर्तें आसान कर दी गई हैं। अब कोई भी घरेलू एअरलाइन विदेश के लिए उड़ान भर सकती है, शर्त यह होगी कि उसे अपने बीस विमानों को या अपनी कुल क्षमता के बीस फीसद को घरेलू उड़ानों के लिए लगाना होगा। घरेलू टिकट रद््द कराने पर पंद्रह दिनों में और अंतरराष्ट्रीय टिकट रद््द कराने पर तीस दिनों में ग्राहकों को पैसा वापस करना होगा। तय सामान यानी पंद्रह किलो से ज्यादा वजन पर घरेलू उड़ान में सौ रुपए प्रति किलो ही शुल्क लगेगा। नई नीति को लेकर स्वाभाविक ही बाजार ने उत्साह दिखाया है; नीति घोषित होते ही कई एअरलाइनों के शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज हुई। पर बाजार के जोश दिखाने के बावजूद नई विमानन नीति की कुछ चुनौतियां भी हैं। घरेलू क्षेत्रीय उड़ानों को किफायती बनाने की कुछ कीमत सरकारी खजाने को चुकानी पड़ सकती है, नुकसान होने की सूरत में सरकार ने अस्सी फीसद तक की भरपाई का भरोसा दिलाया है। यही नहीं, राज्य सरकारों को छोटे शहर के हवाई अड््डे पर विमान के र्इंधन पर लगने वाला वैट एक फीसद या उससे कम करना होगा। फिलहाल दो से पच्चीस फीसद तक वैट लिया जाता है। राज्यों को हवाई अड््डा शुल्क, उप-कर छोड़ना पड़ सकता है या उनमें खासी कटौती झेलनी पड़ सकती है। टिकट की कीमत पर सेवा-कर भी घटाना पड़ सकता है। क्या राज्य इसके लिए तैयार होंगे? क्या कंपनियां किराए की अधिकतम सीमा का नियम आसानी से स्वीकार कर लेंगी? नई विमानन नीति की घोषणा के बाद एक बड़ी चुनौती ढांचागत दुरुस्ती की होगी। आंचलिक हवाई संपर्क योजना को व्यावहारिक रूप देने के लिए बहुत-से अड््डों का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण करना होगा; कई नए हवाई अड््डे बनाने होंगे। जाहिर है, नई विमानन नीति की सफलता का दारोमदार बहुत कुछ राज्यों के सहयोग पर भी निर्भर करता है।
Date: 18-06-16
भारतीय किसान और ब्रेक्सिट
टी. एन. नाइनन
महारानी इलिजाबेथ को हर वर्ष यूरोपीय संघ से करीब 650,000 पाउंड (6 करोड़ रुपये से अधिक)की सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी उन्हें नॉरफक स्थित सैनड्रिंगम एस्टेट के 20,000 एकड़ के खेत के कामकाज के लिए मिलती है। ऐसे कम ही ब्रिटिश नागरिक होंगे जिनको ऐसी सब्सिडी मिलती हो। ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान एक फीसदी से भी कम है। 6.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में करीब 5 लाख लोग ही खेती के काम में लगे हैं। 700 एकड़ के एक खेत को संभालने के लिए बमुश्किल साढ़े तीन लोगों की जरूरत पड़ती है। किसान उपग्रह संचालित ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं जो बिना चालक के एकदम सीधी रेखा में चलते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस)का प्रयोग करके सब्जियां बोई जाती हैं। उनकी कटाई भी मशीनों की मदद से की जाती है। ब्रिटेन की खेती के लिए सालाना यूरोपीय सब्सिडी करीब 30,000 करोड़ रुपये के बराबर है। प्रति खेत और प्रति किसान यह राशि सालाना करीब 6 लाख रुपये पड़ती है।
जो लोग यूरोपीय संघ से अलग होना चाहते हैं उनकी एक दलील यह भी है कि उस स्थिति में ब्रिटेन भारत, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते आदि पर अपने स्तर पर चर्चा और मोलभाव कर सकेगा। अलग होने के एक प्रमुख हिमायती की दलील है कि सन 1973 में यूरोपीय संघ में शामिल होने का अग्रदूत बनने से पहले ब्रिटेन शुल्क मुक्त खाद्य आयात को अनुमति देता था। यह तब था जब वह अपने किसानों को सब्सिडी भी दे रहा था। ऐसे में किसी के मन में यह सवाल उठ सकता है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने के बाद क्या कोई मुक्त व्यापार समझौता कृषि उत्पादों को भी कारोबार के लिए पेश करेगा जबकि उस वक्त तक ब्रिटेन में कृषि की लागत बढ़ चुकी होगी? शायद, लेकिन उसका अर्थ सब्सिडी का अंत नहीं होगा। अगर ब्रिटेन के खेत (महारानी इलिजाबेथ के सैनड्रिंगम समेत) और अन्य इलाके मौजूदा स्थिति में केवल सब्सिडी की बदौलत बचे हुए हैं तो कोई भी सरकार केवल भारत जैसे देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए उसे तिलांजलि नहीं देगी। हमारे देश के तमाम प्रकाशनों के संपादकीय लेखकों में सरकार की कृषि नीतियों की आलोचना करने की आदत है। खासतौर पर कई जटिल, अक्षम और मूल्यों में विसंगति पैदा करने वाले सब्सिडी को लेकर। हमारे देश में कृषि को दी जाने वाली कुल सब्सिडी का आकार यूरोपीय संघ द्वारा ब्रिटेन को दी जाने वाली सब्सिडी से काफी ज्यादा है लेकिन हमारी खेती का आकार भी तो ब्रिटेन की तुलना में 15 गुना है। प्रश्न यह है कि क्या हमें सन 1973 के पहले के ब्रिटेन का अनुसरण करने से लाभ होगा? यानी क्या विसंगति और अक्षमता दूर करने और कृषि क्षेत्र में शुल्क मुक्त व्यापार से? हमें यह भी सुनिश्चित रखना होगा कि किसानों को नकद सब्सिडी भुगतान निरंतर मिलता रहे ताकि वे कृषि जगत की अनिश्चितताओं से निपटते रह सकें। शायद तभी किसान और उपभोक्ता दोनों प्रसन्न हो सकेंगे
Date: 18-06-16
चामलिंग शैली की राजनीति को क्या मिलेगी चुनौती ?
आदिति फडणीस
सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग देश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। वह पांचवीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज संभाल रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी लेकिन उनकी दिल्ली यात्रा मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाईं। लेकिन वह तो इन बातों से बेपरवाह रहते हैं। वह एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो मानव विकास सूचकांक के अधिकांश मानकों में बहुत अच्छी स्थिति में है। ये उपलब्धियां उनके मुख्यमंत्री रहते समय ही हासिल की गई हैं। यह सच है कि उन पर भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। इन मामलों में उनकी दो पत्नियों और उनके बच्चों के अलावा रिश्तेदारों के शामिल होने के भी आरोप लगते रहे हैं। इसके बावजूद सिक्किम के लोगों ने उन्हें बार-बार चुनाव जिताया है। वैसे वर्ष 2014 में हुए पिछले चुनाव में लोगों ने चामलिंग को कुछ चेतावनी भी दी।
Date: 18-06-16
राज्यसभा का चुनाव भी जनता करे
वेदप्रताप वैदिक
अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जो बात लोकतंत्र के लिए कही थी, वही बात उलटकर मैं हमारी राज्यसभा के लिए कहना चाहता हूं। हमारी राज्यसभा राज्यों की सभा नहीं रह गई हैं। वह नेताओं के लिए, नेताओं द्वारा, नेताओं की सभा बन गई है। इसका न तो राज्यों से कोई सीधा संबंध रह गया है और न ही जनता से भी। राज्यसभा नेताओं के जेब का खिलौना बन गई है, इसीलिए भ्रष्टाचार की सारी तरकीबें राज्यसभा के चुनाव में अपनाई जाती हैं। अभी-अभी संपन्न हुए राज्यसभा चुनावों को लेकर कर्नाटक, उत्तरप्रदेश और हरियाणा में जो नौटंकी हुई, उसने नेताओं की छवि तो विकृत की ही, चुनाव आयोग को भी संदेह के घेरे में ला खड़ा किया।
यह स्थिति हरियाणा में ही नहीं, कर्नाटक और उत्तरप्रदेश में भी देखने में आई है। विभिन्न पार्टियों ने अपने-अपने विधायकों को मुअत्तल कर दिया है। उन पर शक है कि उलट-मतदान करने के लिए उन्होंने दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों से करोड़ों रुपए खाए हैं। यह कोई नई बात नहीं है।
हक के इंतजार में किसान
किसानों को उनकी वैधानिक आय से वंचित करना ही भयानक कृषि संकट का एकमात्र कारण है, जो लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ किसान अपनी फसलों की अधिक कीमत मिलने की उम्मीद पाले हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर सरकारें चाहती हैं कि खाद्य महंगाई को नीचे रखने का सारा बोझ किसान उठाएं। किसानों को आर्थिक लाभ की बात तो भूल ही जाएं, दरअसल अनाज पैदा करने के लिए उन्हें एक तरह से दंडित किया जा रहा है। यदि इन बातों पर विश्वास न हो तो इन आंकड़ों पर गौर फरमाएं। 1970 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 51 रुपये था। 2016 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1470 रुपये तय किया गया है। इस बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य में करीब 29 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसी अवधि में सरकारी कर्मचारियों, कॉलेज शिक्षकों-प्रोफेसरों, स्कूल शिक्षकों और मध्यम स्तर के कॉरपोरेट कर्मचारियों के मासिक वेतन में क्रमश: 120 से 150 गुना, 150 से 170 गुना, 280 से 320 गुना और 300 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें मैंने 1970 में प्रचलित सिर्फ मूल वेतन और महंगाई भत्ते की गणना की है। गत 25 साल की अवधि में ही विभिन्न संगठित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों के मासिक वेतन में 120 से 300 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए वेतन वृद्धि का आसानी से मूल्यांकन करने के लिए मूल वेतन में सौ गुना वृद्धि को बेंचमार्क बनाते हैं। यदि किसानों की आय में इसी अनुपात में वृद्धि की गई होती और यदि किसानों की आय की गणना न्यूनतम समर्थन मूल्य में की जाए तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5100 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए था। इस प्रकार किसानों को कम से कम प्रति क्विंटल 3630 रुपये कम मिल रहे हैं। समाज के दूसरे क्षेत्रों के बराबर आय से किसानों को वंचित करने के कारण ही कृषि आज घाटे का सौदा बन गई है। जीवन-यापन के लिए जरूरी आय के अभाव के चलते ही आज किसान कर्ज के दलदल में फंसते गए हैं। बीते बीस सालों से किसानों की आत्महत्या का मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया है।
सातवें वेतन आयोग में एक चपरासी का मूल वेतन करीब 260 प्रतिशत बढ़कर 7000 रुपये से 18000 प्रति महीने हो गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को 108 तरह के भत्ते मिलेंगे, लेकिन किसानों को उनके एमएसपी के अतिरिक्त एक भी भत्ता नहीं दिया जाता है। यदि एमएसपी के साथ सिर्फ चार भत्ते आवास, डीए, स्वास्थ्य और शिक्षा जोड़े जाएं तो भारतीय कृषि की बदहाल तस्वीर अच्छी हो जाएगी। भारतीय कृषि विकास की धुरी बन जाएगी और खेती एक समृद्ध व्यवसाय बन जाएगी। लेकिन जैसे ही कोई उच्च एमएसपी की मांग करने लगता है वैसे ही अर्थशास्त्री खाद्य महंगाई की ऊंची दर का डर दिखाने लगते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जिन लोगों को महंगाई भत्ता दिया जाता है उनको खाद्य महंगाई से अप्रभावित रखने के लिए किसानों को क्यों कष्ट दिया जाना चाहिए? खाद्य कीमतों को नीचे रखने का बोझ औसत उपभोक्ता क्यों नहीं साझा कर सकते? आखिर अर्थशास्त्री इस बात को क्यों नहीं समझते कि देश में किसान ही एक ऐसा समुदाय है जिसे उसकी वैधानिक आय से वंचित किया जा रहा है? किसानों को कृषि कल्याण के नाम पर लिए जाने वाले 0.5 प्रतिशत सेवा कर की जरूरत नहीं है। उन्हें समाज के दूसरे हिस्से के समान ही उच्च एमएसपी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो वित्त मंत्रालय भी सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार करे। एक छोटे हिस्से को संतुष्ट करने के लिए एक बड़े हिस्से की बलि नहीं दी जा सकती है। किसानों के कल्याण के लिए उपकर और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग-इससे असमानता की गंध आती है।
यह किसान आय आयोग गठन करने का सही समय है। मेरा सुझाव है कि सरकार एमएसपी की तय 1470 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी करे। 3630 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शेष रकम को सरकार सीधे धान उत्पादकों के बैंक खाते में जमा करा दे। चूंकि जनधन योजना के तहत सभी किसानों के बैंक खाते खुल गए हैं लिहाजा इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इससे खाद्य महंगाई भी नियंत्रण में रहेगी और साथ ही किसानों की आय में असुरक्षा का मुद्दा भी सुलझ जाएगा। यदि सरकार सातवें वेतन आयोग के जरिए 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 50 लाख पेंशनधारियों पर सालाना 1.02 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च करने को तैयार है तो इसी तरह धान उत्पादकों के लिए इतनी राशि उपलब्ध क्यों नहीं की जा सकती है। किसानों के हाथों में जितना पैसा होगा उतनी ही ज्यादा मांग पैदा होगी। यह मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास के लिए पहली शर्त है, जो कि पर्याप्त घरेलू मांग के अभाव में अभी पीछे छूट रहा है। मेरी समझ से यह कदम प्रधानमंत्री की सबका साथ सबका विकास की भावना को चरितार्थ करेगा।
[लेखक देविंदर शर्मा, कृषि और खाद्य नीतियों के विश्लेषक हैं ]
Date: 18-06-16
सबसे बड़ा चुनाव सुधार
भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने में हम सभी गौरवान्वित होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी आठ जून को अमेरिकी संसद के संयुक्त अधिवेशन में इसका उल्लेख किया। लेकिन क्या बड़ा लोकतंत्र होना ही गौरव की बात है? क्या हमें एक अच्छा लोकतंत्र होने का प्रयास नहीं करना चाहिए? ज्यादातर लोग इसी बात से खुश हो जाते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से हमारे यहां बराबर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते रहे हैं। चुनाव-आयोग, केंद्रीय सरकार, राज्य-सरकारें, प्रशासन और जनता सभी को इस पर गौरव होना स्वाभाविक है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि चुनाव लोकतंत्र की धड़कन तो है, उसके जीवंत होने का प्रमाण तो है, पर उसके स्वस्थ, संपन्न और गुणवत्तापूर्ण होने का प्रमाण नहीं। चुनाव को लोकतंत्र का पर्याय नहीं कहा जा सकता। हमें चुनावों से आगे जाना होगा, हमें चुनावों द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक शैली पर काम करने वाली सरकारों से सुशासन और विकास की नई अपेक्षाएं करनी होंगी। हमें ऐसी सरकारों से यह दरकार होगी कि वे देश में एक नई राजनीतिक-संस्कृति के माध्यम से दक्ष, प्रभावी और मितव्ययी प्रशासन स्थापित करें जो पारदर्शी, स्वच्छ एवं संवेदनशील हो।
इसी संदर्भ में देश में लोकसभा, विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों का चुनाव एक साथ करने का सुझाव महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो चुनाव-सुधारों की चर्चा प्राय: होती रहती है, लेकिन हाल में संसदीय-समिति ने दिसंबर 2015 में अपने प्रतिवेदन में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। इस पर विधि-मंत्रालय ने चुनाव आयोग से राय मांगी। आयोग ने मई के प्रथम सप्ताह में इस पर अपनी सहमति दे दी। गौरतलब है कि विगत लोकसभा चुनावों में भाजपा ने भी इसे अपने घोषणापत्र में रखा था और मार्च 2016 में मोदी ने भाजपा की बैठक में देश में सभी चुनावों को एक साथ कराने की हिमायत भी की। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी इस विचार के समर्थक रहे हैं और 28 मई 2010 के अपने ब्लॉग में उन्होंने यह भी लिखा कि कुछ समय पूर्व एक रात्रि भोज के दौरान इस मुद्दे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी भी एक साथ चुनावों के विचार से सहमत दिखे। संविधान लागू होने के बाद चार बार (1951, 1957, 1962, 1967) लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। लेकिन 1967 में आठ राज्यों-बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मद्रास (तमिलनाडु) और केरल में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनने से संपूर्ण संघीय ढांचे पर कांग्रेस का एकछत्र वर्चस्व खत्म होने की शुरुआत हो गई। गैर-कांग्रेसी सरकारों को भंग करके उन राज्यों में मध्यावधि चुनाव कराए गए। तबसे लेकर आज तक एक साथ चुनावों का चक्र बन नहीं पाया जिससे हर समय देश में कहीं न कहीं चुनाव चलता ही रहता है।
एक साथ चुनाव करने का विचार तो अच्छा है, लेकिन उसमें अनेक बाधाएं हैं जिन्हें दूर करने के बारे में राष्ट्रीय सहमति जरूरी होगी। सबसे बड़ी बाधा संवैधानिक है। संविधान ने हमें लोकतंत्र का संसदीय-मॉडल दिया जिसमें यद्यपि लोकसभा और विधानसभाएं पांच वषो्र्रं के लिए चुनी जाती हैं, लेकिन अनु. 85 (2) ब के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को और अनु. 174 (2) ब के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को पांच वर्ष के पूर्व भी भंग कर सकते हैं। अनु. 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और विधानसभाओं को आपातकाल की स्थिति में उनके कार्यकाल के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अनु. 352 के तहत युद्ध, वाह्य-आक्रमण और सशस्त्र-विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय-आपात लगाकर लोकसभा के कार्यकाल को पांच-वर्ष के आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनु. 2 के अंतर्गत संसद किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है और अनु. 3 द्वारा कोई नया राज्य बना सकती है, जिनके चुनाव अलग से कराने पड़ सकते हैं। यदि नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव भी संसद और विधानसभाओं के साथ कराने का सुझाव भी जोड़ दिया जाए तो संविधान के भाग 9 अनु. 243 में भी कई संशोधन करने पड़ेंगे। ऐसे संवैधानिक संशोधनों में आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होगी।
ज्यादातर यूरोपीय देशों ने संसद के निर्वाचित सदन के स्थायित्व का मॉडल अपनाया है और इंग्लैंड, जहां से हमने अपने संविधान का मॉडल लिया, वहां भी कॉमन सभा का कार्यकाल निश्चित करना सोचा जा रहा है। इस पूरी योजना में संसद द्वारा सरकार (कार्यपालिका) हटाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बल्कि सरकार (कार्यपालिका) द्वारा संसद और विधानसभाओं को हटाने पर प्रतिबंध लग जाएगा। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भारत में ऐसा हो पाना संभव नहीं लगता। लेकिन एक साथ चुनाव कराने के फायदे बहुत हैं। एक, पूरे देश में केवल एक ही मतदाता सूची होगी। अभी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों की अलग-अलग मतदाता सूचियां है। अक्सर मतदाता का नाम एक सूची में होता है, लेकिन दूसरी सूची में नहीं होता, जिससे वह मतदान से वंचित हो जाता है। दो, देश को प्रतिवर्ष चुनाव से राहत मिलेगी और सरकारों व जनता को पांच वर्ष तक अपने-अपने काम पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा। तीन, रोज-रोज के चुनावों से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। कहीं मॉडल-कोड ऑफ कंडक्ट के कारण विकास रुकता है तो कहीं नौकरशाह चुनावों का बहाना बनाकर विकास कार्यों से बचते हैं।
चार, देश में चुनावों में हिंसा रोकना एक बड़ी चुनौती होती है, जिसमें पुलिस, अर्ध-सैनिक बल और कभी-कभी सेना भी बुलानी पड़ती है। यदि पांच साल के बाद चुनाव हों तो उनको भी बड़ी राहत मिलेगी। पांच, रोज-रोज के चुनावों में सबसे ज्यादा नुकसान स्कूल-कॉलेज के बच्चों का होता है, उनकी पढ़ाई में व्यवधान आता है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक तो अक्सर मतदाता सूची बनाने से लेकर चुनाव में मतगणना तक सभी कार्यों के लिए बाध्य किए जाते हैं, जो देश के भावी-कर्णधारों के साथ एक खिलवाड़ है। और इसके अलावा देश की विविधता के चलते चुनावों में सांप्रदायिक सद्भाव बिगडऩे और जातीय-उन्माद बढऩे की भी संभावना बहुत बढ़ जाती है, जो सरकारों के लिए सिरदर्द और समाज के लिए अभिशाप बन जाती है। यदि वास्तव में संसद, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल और जनता इस सुझाव पर संजीदगी से विचार करें तो पूरे देश में सभी संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव एक साथ जरूर कराए जा सकते हैं। इससे भारतीय लोकतंत्र न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाएगा, बल्कि संभवत: वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बनने की दिशा में एक मजबूत कदम भी बढ़ाएगा।
[ लेखक डॉ. एके वर्मा, सेंटर फॉर द स्टडी आफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं ]