
12-01-2021 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Pride And Prejudice
Govt must give ASHAs, Anganwadi volunteers rights, benefits due as workers
Neetha N., [ The writer is professor, Centre for Women’s Development Studies ]
COVID-19 has given visibility to Accredited Social Health Activists (ASHA) and Anganwadi workers — women “volunteers” attached to a government scheme or employed on a mission mode — who are frontline warriors in the battle against the pandemic. In India, there are about a lakh ASHA workers, 1.3 million Anganwadi workers and another 1.2 million Anganwadi helpers, of them women. As the response to the pandemic required localised approaches, services of community workers became useful, given their robust contacts at the grass roots. During the lockdown, when there was uncertainty and fear of the virus, these women became the connecting link between the community and the state machinery.
However, these community worker-volunteers are a perfect example of how the state devalues women’s work, especially the labour of those involved in care work. The stereotype that persists of women’s ability and their inbuilt consciousness to understand other fellow beings’ feelings, especially other women, makes them perfectly suitable to be recruited as community workers. This explains the presence of a large number of women in community-based programmes across the world. But, in India, there is a refusal to recognise this “all women workforce” as workers providing labour. They are classified as “honorary workers”, denied minimum wages, leave and other conditions that work entails. Sugar-coated in the superior value-domain of women as the embodiment of care service providers, the state prefers to call them “volunteers”. The assumption that women’s care and emotional labour is outside the mundane world of markets is often evoked to pay these overworked workers just an honorarium. But, even in the best paid states, this honorarium is not even close to the government-mandated minimum wages offered to workers doing comparable jobs. Many petitions have been submitted by community workers and their unions demanding recognition as workers. During the pandemic, Anganwadi, ASHA and National Health Mission workers had a two-day nationwide strike demanding safety, insurance, risk allowance and fixed wages. The Parliamentary Standing Committee on Labour also recommended formalising the work of community workers. But the government has not relented.
The contributions of these women workers have been taken for granted by the community, an outcome of the social understanding of women’s labour and its invisible status. The one positive aspect of their work is that the society recognises them as a part of the state machinery. This enables many women to negotiate patriarchal restrictions and norms of mobility. However, mobility of women workers is often a contested terrain and gets defined and controlled as per social norms.
Now that the pandemic is moving to the next stage with the coming of the vaccine, these volunteers will be the first to be forgotten both by the state and society at large. From the glorified position of corona warriors, they will slowly retreat to their old unrecognised identity and sphere of neglect.
It is high time that the state recognises the contributions of these women and accept them as workers. This could help in resolving the larger issue of devaluation of women’s work and their secondary status as workers. The exclusionary tendencies of the labour market, rooted in the social understanding of women’s work, where the state is an active participant has not only restricted women’s employment prospects, but has also created silos of women’s employment such as paid domestic work. The declining women’s workforce participation has been a matter of concern even before COVID. Wages and conditions of work of women care workers are matters of concern and the state apathy to recognise the growing sectors of women’s employment such as domestic work has a long history.
With all field reports and CMIE data pointing to a deeper crisis in female employment during the pandemic, state intervention is much needed. The recognition of ASHA and Anganwadi volunteers as workers, even if it is contractual, will thus not only be a tribute to their contribution during the pandemic, but also an opportunity to shake the structural understanding of women’s labour and their status in the labour market. Recognition of care work in the public sphere could also help in unsettling the gendered and unequal division of house work and unpaid care burden.
Reframing India’s foreign policy priorities
Apart from an ideational restructuring, prudent plans, achievable objectives and a line of continuity are a must
M.K. Narayanan is a former National Security Adviser and a former Governor of West Bengal
The year 2021 should see a cementing of the many trends that had their genesis in 2020. Leadership change in the United States is perhaps the most awaited change, but is unlikely to bring about a major power shift in the international arena. Even before the changeover, and despite the promise of a Biden presidency to invigorate the U.S.-Europe axis, Europe has turned its back on the U.S. and revived its China links, by ‘concluding in principle the negotiations for an EU-China Comprehensive Agreement on Investment’. In one swift move, Europe has thus shattered all hope that China would remain ostracised in 2021.
Many countries will now find themselves scrambling for cover. India which has greatly curtailed its relations with China since April 2020, (in the wake of Chinese aggression in Eastern Ladakh) will find itself ‘out on a limb’, with many countries likely to seek closer economic relations with China now.
A stronger China
The year 2021, hence, begins on a triumphal note for China and China’s Supreme Leader, Xi Jinping. China is about the only major country which had a positive rate of growth at the end of 2020, and its economy is poised to grow even faster in 2021. Militarily, China has further strengthened itself, and now seeks to dominate the Indo-Pacific Ocean with its announcement of the launch of its third aircraft carrier in 2021. Simultaneously, it is seeking to strengthen its military coordination with Russia. Consequent on all this, and notwithstanding Chinese intransigence in several matters including its heavy-handed actions in Hong Kong and Uighur, China’s position across Asia is, if anything, stronger than in 2020. News emanating from China is that President Xi will further cement his position, both as Party leader and as President during 2021, despite internecine tensions within the Communist Party of China. China is, hence, unlikely to concede any ground to its opponents across the world in 2021, a fact that India will need to reckon with. It cannot expect any Chinese concessions in Eastern Ladakh, until India ‘makes amends’.
Economy first for Europe
The new year will be dominated by strong authoritarian leaders like Xi Jinping in China, Vladimir Putin in Russia, and Recep Tayyip Erdoğan in Turkey. International politics may not be very different from that in 2020, but any hope that the Compact of Democracy would emerge stronger will need to be eschewed. Europe, minus Britain following Brexit, and the retirement of Germany’s Angela Merkel, could become even less relevant in world affairs. The China-EU Investment Treaty which saw Europe capitulating to China’s brandishments is an indication that Europe values its economy more than its politics.
Major changes are afoot in Eurasia and West Asia which could lead to significant shifts. Russia is beginning to display greater interest in the affairs of countries on its periphery and, together with strengthening ties with China and reaching an entente with Turkey, this seems to signal reduced interest in countries such as India. In West Asia, the Abraham Accords, leading to a realignment of forces in the Arab world, have sharpened the division between the Saudi Bloc and Iran-Turkey. Despite the hype surrounding the Abraham Accords, the situation, however, remains fluid and has not reduced the risk of a confrontation between Iran and Israel. This does pose problems for India, since both have relations with it. Meanwhile, China demonstrates a willingness to play a much larger role in the region, including contemplating a 25-year strategic cooperation agreement with Iran.
Saudi Arabia could find the going difficult in 2021, with a Biden Administration taking charge in Washington. The healing of wounds among the Sunni Arab states in the region should be viewed as a pyrrhic victory at best for Saudi Arabia. One by-product of this could be a sharpening of hostilities between the Sunni and Shia camps. Given the strategic flux in the region, Iran could well be tempted to use its nuclear capability to enhance its position, confident that the West may be unwilling to challenge it at this juncture.
India isolated
At the start of 2021, India seems the odd man missing as far as these developments are concerned. No breakthrough in Sino-Indian relations has, or is likely to occur, and the confrontation between Indian and Chinese armed forces is expected to continue. India currently plays no significant role in West Asia. India-Iran relations today lack warmth. In Afghanistan, India has been marginalised as far as the peace process is concerned. While India’s charges against Pakistan of sponsoring terror have had some impact globally, it has further aggravated tensions between the two neighbours, and in the process, also helped Pakistan to cement its relations with China. While hostility between India and Nepal appears to have reduced lately, relations continue to be strained. Through a series of diplomatic visits, India has made valiant efforts to improve relations with some of its neighbours such as Bangladesh, Myanmar and Sri Lanka, but as of now worthwhile results are not evident. One key takeaway is that as India-China relations deteriorate, India’s neighbours are not averse to taking sides, increasing India’s isolation.
Whether India’s perceived marginalisation from global mainstream events as we enter 2021 signifies a sharp drop-off in its foreign policy capabilities is, no doubt, debatable. India’s foreign policy objectives are to widen its sphere of influence, enhance its role across nations, and make its presence felt as an emerging power in an increasingly disruptive global system. It is a moot point though whether any of these objectives has been achieved. Today, India’s voice and counsel are seldom sought, or listened to. This is a far cry from what used to happen previously. India will serve as the president of the powerful UN Security Council for the month of August, 2021, but if it is to make a real impact, it must be seen to possess substantial weight to shape policies, more so in its traditional areas of influence.
Diplomacy and perceptions
Many explanations could be available for this state of affairs. Admittedly, our diplomats conduct their activities with a high degree of competence, but they are possibly hampered by other factors. One, could be the kind of policy choices the country has adopted in the recent period, which have possibly altered the perception of India in certain quarters. There is again a perception that India’s closeness to the U.S. has resulted in the weakening of its links with traditional friends such as Russia and Iran, impacting the country’s image. Perhaps the most relevant explanation could be the shifting balance of power in the region in which India is situated, notably the rise of China, and the enlarging conflict between the two biggest powers in Asia, compelling many nations to pick sides in the conflict.
A less obvious, but perhaps more relevant aspect, could also be that India’s foreign policy suffers from an ideational vacuum. It is not the sharp decline in the economy, problems caused on account of the pandemic, or the growing polarisation in values across nations and societies, but more possibly India’s inability or failure in the ideational realm that lies at the root of our foreign policy inadequacies.
More misses than hits
Currently, India remains isolated from two important supranational bodies of which it used to be a founding member, viz., the Non-Aligned Movement (NAM) and the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). Efforts to whip up enthusiasm for newer institutions such as the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC), have hardly been successful. India has opted out of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) (a majority of Asian countries are members), and failed to take advantage of the RIC, or the Russia, India and China grouping, even as relations with Russia and China have deteriorated. On the other hand, India’s foreign policy imperatives, across Asia and South Asia in particular, today seem to be a mixture of misplaced confidence, sometimes verging on hubris (as in the case of Nepal), a lack of understanding of the sensitivities of neighbours such as Bangladesh and long-time friends (such as Vietnam and Iran), and according excessive importance to the policy needs and pressures of nations such as the U.S. There is possibly a misplaced perception in much of Asia that the India of today is not unwilling to sacrifice its strategic autonomy under U.S. pressure.
As part of the ideational restructuring of India’s foreign policy, what is urgently required, apart from competent statecraft, is the adoption of prudent policies, pursuit of realistically achievable objectives, and, above all, a demonstration of continuity of policy, irrespective of changes in the nature of the Administration. These may be time consuming, but are a surer recipe for success in attaining foreign policy objectives.
लोगों के हाथ में पहुंचना होगा पैसा
भरत झुनझुनवाला, ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )

तीसरा सुझाव जीएसटी की दर का है। वर्ष 2019-20 में केंद्र को इस श्रोत से 6.1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। इसकी दर घटाकर इसे भी चार लाख करोड़ रुपये के संग्रह वाले लक्ष्य से जोड़ा जाए। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी और मांग बढ़ेगी। चौथा सुझाव आयात कर की दर का है। वर्ष 2019-20 में सरकार को इससे 60 हजार करोड़ रुपये मिले। इसकी दर तीन गुना बढ़ा देनी चाहिए जिससे कि इससे करीब 2 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिले। आयात कर बढ़ाने से घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बाजार में मांग बढ़ेगी और घरेलू अर्थव्यवस्था चल निकलेगी।
पांचवां सुझाव केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी का है। वर्ष 2019-20 में केंद्र को इससे 2.5 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिला। इसकी दर बढ़ा दी जाए जिससे कि इससे भी चार लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिले। इस मद में अधिकांश हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थों का होता है। उनके दाम बढ़ने से आम आदमी को झटका लगेगा, लेकिन इसकी भरपाई जीएसटी की दर घटाने एवं अन्य तरीकों से संभव हो सकती है। इससे पेट्रो उत्पादों की मांग घटेगी और उनके आयात में कमी आएगी। विदेशी व्यापार संतुलित होगा। रुपये का मूल्य चढ़ेगा। इनके अतिरिक्त केंद्र को अन्य मदों से 4.3 लाख करोड़ और ऋणों से 7.7 लाख करोड़ रुपये मिले। इन्हें यथावत रहने दें। इस प्रकार 2019-20 में सरकार का जो बजट 27 लाख करोड़ रुपये रहा उसकी तुलना में आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार को 30 लाख करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध हो जाएगी।
अब खर्च की तरफ ध्यान दें। रक्षा बजट 2019-20 में चार लाख करोड़ रुपये था। इसे बढ़ाकर सात लाख करोड़ रुपये कर देना चाहिए, क्योंकि देश की सीमाओं पर संकट विद्यमान है। 2019-20 में संचार एवं विज्ञान के क्षेत्रों में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए जिसे पांच गुना बढ़ाकर तीन लाख करोड़ रुपये कर देना चाहिए ताकि देश में नई तकनीकों के आविष्कार को प्रोत्साहन मिले। गृह मंत्रालय का खर्च 2019-20 में 1.4 लाख करोड़ रुपये था। इसे पूर्ववत बनाए रखा जाए, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य पर सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जिसे कायम रखा जाए। इसमें परिवर्तन यही करना चाहिए कि विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को समाप्त करके बचाई रकम को कोविड तथा अन्य बीमारियों पर शोध में लगा देना चाहिए।
इनके बाद दो प्रकार के अन्य मंत्रालय आते हैं। पहले बुनियादी संरचना वाले मंत्रालय जैसे सड़क, बिजली, रेलवे इत्यादि। इनके खर्चों को आधा कर देना चाहिए और हाईवे आदि के निर्माण को एक वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए। अभी देश के लिए सबसे अधिक आवश्यक बाजार में मांग उत्पन्न करना है। मंत्रालयों की श्रेणी में दूसरे मंत्रालय कल्याणकारी उद्देश्य से जुड़े हैं। जैसे खाद्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि। उनके खर्चों को भी आधा कर देना चाहिए। इन मंत्रालयों का काम केवल सार्वजनिक कार्यों को संपादित करने का रह जाना चाहिए। केंद्रीय विद्यालयों का निजीकरण करके भी रकम बचाई जा सकती है। इन दोनों प्रकार के सभी अन्य मंत्रालयों पर 2019-20 में 20 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए थे जिसे घटाकर 10 लाख करोड़ कर देना चाहिए।
उपरोक्त सभी खर्चों का योग 22 लाख करोड़ होता है। वहीं सरकार की आय हमने 30 लाख करोड़ आंकी थी। ऐसे में शेष आठ लाख करोड़ की जो रकम बचती है उसे देश के प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते में सीधे प्रति माह हस्तांतरित कर देनी चाहिए। इस रकम से 140 करोड़ लोगों को प्रतिमाह करीब 500 रुपये दिए जा सकते हैं जो पांच व्यक्तियों में परिवार में 2,500 रुपये तक हो सकते हैं। इसे ‘हेलीकॉप्टर मनी’ कहा जाता है। मानो किसी हेलीकॉप्टर से आपके घर में रकम पहुंचा दी जाए। आठ लाख करोड़ की इस विशाल राशि के सीधे लोगों के हाथ में पहुंचने से मांग में तेजी आएगी। इसके साथ ही यदि आयात कर भी बढ़ा दिया जाए तो बढ़ी मांग की पूर्ति के लिए घरेलू उत्पादन में स्वत: बढ़ोतरी होगी। इससे रोजगार भी बढ़ेंगे। वहीं आम लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की बंदी से हुए नुकसान की भरपाई प्रत्यक्ष मदद से पूरी हो जाएगी।
मूल बात यही है कि सरकारी खर्च को उच्च वर्ग से हटाकर आम वर्ग की ओर मोड़ना चाहिए। इससे विदेशी वस्तुओं के उपभोग में कमी आएगी। इसका प्रभाव यही होगा कि बाजार में घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ेगी जिससे घरेलू उत्पादन, रोजगार सृजन और मांग का सुचक्र स्थापित होगा। इन कदमों से हम 10 से 12 प्रतिशत तक आर्थिक विकास दर हासिल कर सकते हैं। सरकार को तय करना होगा कि राजनीतिक दृष्टि से उसके लिए उच्च वर्ग का वित्तीय समर्थन अधिक लाभप्रद है या आम जनता के वोट। हेलीकॉप्टर मनी के वितरण से सरकार को उसी प्रकार का राजनीतिक लाभ होगा जैसा कांग्रेस को 2009 के चुनाव में मनरेगा लागू करने से हुआ था।
Date:12-01-21
आत्म-उन्नति के पथप्रदर्शक विवेकानंद
शंकर शरण, ( लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर हैं )
स्वतंत्र भारत की शिक्षा में भारतीय ज्ञान का लोप होता गया है। बहुतेरी मूल्यवान सीखों से नई पीढ़ियां वंचित होती रही हैं। उलटे आधुनिक शिक्षा के नाम पर तो उसके बारे में भ्रामक धारणाएं भी बना दी गई हैं। जैसे-उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि को ‘धर्मग्रंथ’ कहा जाता है, जबकि वे ज्ञानग्रंथ हैं। ऐसी ही एक भ्रामक धारणा स्वामी विवेकानंद के बारे में बना दी गई है। उन्हें धर्मगुरु बताया जाता है, जबकि वह महान शिक्षक थे, भारतीय ज्ञान-परंपरा के व्याख्याता थे। अमेरिका और यूरोप में उन्होंने योग-वेदांत के ही व्याख्यान दिए, जिनसे उन्हें ख्याति मिली। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में उन्हें महान शिक्षक के बजाय ‘रिलीजियस’ जैसी श्रेणी में रख दिया गया। मानो उनकी शिक्षाओं की बच्चों, युवाओं को आवश्यकता नहीं, जबकि सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। बरसों अमेरिका और यूरोप में कीर्ति पताका फहराने के बाद जब विवेकानंद भारत लौटे तो देशभर में घूम-घूमकर उन्होंने आमजनों के बीच व्याख्यान दिए। कोलंबो, मद्रास से लेकर ढाका, लाहौर तक स्वामी जी के व्याख्यान लाखों लोगों ने सुने। उनका संग्र्रह ‘कोलंबो से अल्मोड़ा तक’ अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है। हिंदी में उसका अनुवाद महाप्राण कवि निराला ने किया था। उन व्याख्यानों का संक्षिप्त संस्करण ‘युवकों के प्रति’ शीर्षक से रामकृष्ण आश्रम ने प्रकाशित किया है। वह प्रत्येक भारतीय के लिए पठनीय है। विवेकानंद ने ऐसी कई सीखें दीं जो दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं। उन्होंने कहा था कि किसी कठिनाई से भागें नहीं, बल्कि सीधे उसका सामना करें तो कठिनाई तुरंत हल्की लगने लगेगी। कभी किसी बाहरी मदद की आस न करें, क्योंकि सारी शक्ति आपके अंदर ही है। अब तक जीवन में उसी से सब कुछ उपलब्ध हुआ है। भावनाओं में न बहें, क्योंकि आवेश और तीव्रता में जाने से शक्ति का निरर्थक क्षय होता है। किसी से व्यवहार करते हुए एकत्व की ओर बढ़ने वाले काम करें, निकटता लाने वाली बात बोलें, न कि दुराव बढ़ाने वाली। काम करते हुए सभी कर्मफल श्रीकृष्ण और माता पार्वती को र्अिपत करते रहें। यह सोच कर कि यह उनका काम है।
यहां आपको शंका हो सकती है कि सांसारिक लोग ऐसा निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं? विवेकानंद ने इसे इस तरह समझाया है। मान लीजिए एक सेविका अपने मालिक के बच्चे का प्रेम भाव से लालन-पालन करती है, परंतु यदि मालिक उसे काम से हटा दे या वही कोई नया काम पकड़ ले तो वह चिंता नहीं करती कि अब बच्चे का क्या होगा, कैसे होगा। वह अपनी गठरी लेकर नए काम पर चली जाती है। सांसारिक लोगों को भी इसी भाव से हर काम करना चाहिए। यदि आसक्ति रखे बिना हम सारे काम करते जाएं, तब कभी क्लेश नहीं होगा अथवा नगण्य होगा। विवेकानंद ने आगे कहा है कि कोई काम करते हुए दुविधा में न पड़ें। अच्छे-बुरे की चिंता छोड़कर कर्म करें, क्योंकि भलाई-बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्वंद्व ही जीवन है। बिना विकार के कर्म असंभव है। अत: अपनी ओर से जानते-बूझते अनुचित कार्य न करें। बाकी अपने कर्म के फलाफल की परवाह छोड़कर कार्य करें। उसे राम जी पर छोड़ दें।
वस्तुत: अनासक्त होकर कार्य करना ही व्यावहारिक है। विवेकानंद ने कहा है कि किसी चीज, विचार, व्यक्ति से आसक्ति न रखें। केवल कर्तव्य भाव रखें। मन को अपने अधीन रखें। अपने परिवार और संपत्ति के प्रति भी उसके मालिक नहीं, बल्कि अवधिबद्ध वेतनभोगी व्यवस्थापक जैसा भाव रखें, क्योंकि यही सत्य है। उपनिषद के आरंभ में ही है, ‘कस्य स्विद धनम्’। अर्थात धन किसी का नहीं है। किसी मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके असंख्य जन्मों में एक है जो पलक झपकते ही व्यतीत हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलता कि कब वृद्ध हो गए। आपका वर्तमान घर एक धर्मशाला भर है। आपके परिवारजन सांयोगिक पड़ोसी मात्र हैं, जिनसे दूर होना अनिवार्य है। अत: उन्हेंं प्यार करें, उनका ध्यान रखें, परंतु उन्हें ‘मेरा’ न कहें। स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि किसी का अत्यंत मूल्यवान चित्र जल जाता है तो आपको कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि वह ‘आपका’ नहीं। अर्थात ये ‘मैं एवं मेरा’ ही सारे क्लेश की जड़ हैं। इस भावना से मुक्त होकर ही हुए हम आनंदित रह सकते हैं, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल रोज कुछ देर स्वाध्याय, योगाभ्यास और चिंतन से हमारे भीतर सच्ची कर्म भावना विकसित हो जाएगी। स्वामी जी के अनुसार बिना स्वार्थ किया गया प्रत्येक कार्य हमारे पैरों की एक बेड़ी को काट देता है। ध्यान से देखें तो यही सहज मानवीय स्वभाव है। मनुष्य की सारी छटपटाहट अंतत: मुक्ति पाने के लिए है। मानव जिस शुद्ध, अनश्वर, असीम, अनादि का अंश है, उसी से पुन: मिल जाने की इच्छा उसके अंतरतम में कहीं दबी है। विवेकानंद उसे सदैव स्मरण रखने के लिए रानी मदालसा की पौराणिक कथा स्मरण कराते हैं। वह अपने नवजात पुत्र को आरंभ से ही गीत गाकर शिक्षा देती थी कि हे पुत्र, तुम शुद्ध, बुद्ध, निरंजन हो, तुम्हें क्रिया चिंता, क्या क्लेश! विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक बच्चे में जन्म से ही इस गीत का भाव भर दिया जाना चाहिए ताकि वह आजन्म आनंदित रह सके।
योग-वेदांत की संपूर्ण शिक्षा मनुष्य को सच्चा कर्मयोगी बनाने की है। उससे अधिक व्यावहारिक शिक्षा कोई नहीं हो सकती। किसी भी आयु में, कोई भी रोजगार करते हुए, उसकी उपयोगिता यथावत है। वेदांत कोई ‘फेथ’ वाला रिलीजन नहीं, जर्मन भाषा वाला ‘साइंस’ है। जैसे शरीर और भौतिक जगत के लिए भौतिकी, रसायन, कृषि आदि का विज्ञान है, उसी तरह आत्मिक जगत के लिए योग-वेदांत का विज्ञान है। इसीलिए वह शुद्ध व्यावहारिक ज्ञान है। स्वामी विवेकानंद ने इसी शिक्षा से पूरी दुनिया को विस्मित कर दिया था। हम उसे विस्मृत करके अपनी ही हानि करते रहे हैं।
 Date:12-01-21
Date:12-01-21
कृषि कानून: सर्वोच्च विडंबना
संपादकीय
देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार और किसान नेताओं के समक्ष एक ऐसा विकल्प प्रस्तुत किया है जो उन्हें तीनों कृषि कानूनों को लेकर बनी गतिरोध की स्थिति से बचने का अवसर देता है। ये तीनों कृषि कानून, दशकों पुराने कृषि विपणन कानूनों समेत कृषि क्षेत्र में तमाम आवश्यक सुधार लाने के लिए बनाए गए हैं। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाले तीन न्यायाधीशों के पीठ ने इन कानूनों की वैधता से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि बेहतर होगा कि केंद्र सरकार इन कानूनों के क्रियान्वयन पर तब तक रोक लगा दे जब तक न्यायालय इस विषय पर चर्चा के लिए समिति का गठन नहीं करता। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो न्यायालय को ऐसा करना होगा। गत माह पीठ ने संकेत दिया था कि वह सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाएगा जो गतिरोध समाप्त करने के रास्ते तलाश करेगी। मौजूदा हालात में ये दोनों हल समझदारी भरे प्रतीत होते हैं। परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर सरकार ने पहले ये कदम क्यों नहीं उठाए। आखिरकार सरकार हमेशा से प्रतिस्पर्धी हितों के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए समितियों का गठन करने का रास्ता अपनाती रही है। बहरहाल अब यह प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आया है और दोनों पक्षों को यह अवसर देता है कि वे सम्मानजनक ढंग से इस गतिरोध को समाप्त करें। अस्थायी ही सही लेकिन गतिरोध समापन के ऐसे उपाय की आवश्यकता थी। यह विवाद दोनों पक्षों के लिए अस्थिरता लाने वाला है और सरकार के लिए ऐसी राजनीतिक जटिलताएं पैदा कर सकता था जिनसे वह बचना चाहेगी क्योंकि वह इस महीने के अंत तक कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाली है।
सर्वोच्च न्यायालय की घोषणाओं में तीन बातें ध्यान देने लायक हैं। पहली है उसके रुख में दिख रही कड़ाई। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना वक्तव्य इस तथ्य के आधार पर दिया है कि किसी भी किसान प्रतिनिधि ने कानूनों को बेहतर नहीं बताया है। तीसरा, न्यायालय ने कानूनों पर रोक नहीं लगाई है बल्कि उसने कहा है कि इनके क्रियान्वयन को स्थगित रखा जाना चाहिए। तीनों बातें बताती हैं कि इस विषय पर सरकार शायद जनता का समर्थन गंवा चुकी है, भले ही इन कानूनों के पक्ष में कितनी भी मजबूत आर्थिक दलीलें क्यों न हों। यदि सरकार ने संसद में अपने भारी बहुमत पर भरोसा करते हुए कानून को पारित नहीं किया होता तो शायद न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर चिंतित लोग शायद इनके व्यापक प्रभाव को समझ पाते। इसके बजाय सरकार ने बेहद हड़बड़ी के साथ इन कानूनों को पारित किया। संसद का वह सत्र कोविड-19 के कारण सीमित कर दिया गया था और इस पर सांसदों के बीच समुचित चर्चा भी नहीं हो सकी।
इसके अलावा सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की बड़ी वजह बन चुकी पराली जलाने वाले किसानों को जुर्माने से छूट और बिजली शुल्क दरों में इजाफा स्थगित करने वाले कदम उठाने पड़े। यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने पिछले महीने की घोषणा के मुताबिक कानूनों को स्थगित करके समिति के गठन की दिशा में पहल क्यों नहीं की। अब जबकि न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में समिति के गठन की घोषणा कर दी है तो यह पहल सरकार के हाथ से निकल गई। समिति गठन की पहल सर्वोच्च न्यायालय ने कर दी है तो सरकार ने कार्यकारी शक्ति न्यायपालिका के हाथ गंवा दी। कोयला, दूरसंचार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरह इस मामले में भी कार्यपालिका क्षेत्र में न्यायपालिका का यह दखल अच्छा नहीं। मात्र एक खरीदार वाली पुरातन व्यवस्था को बदलने का विशिष्ट अवसर कमजोर हुआ है।
Date:12-01-21
लोकतंत्र बनाम आर्थिक सुधारों पर जारी चर्चा
के पी कृष्णन, ( लेखक भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं एनसीएईआर में प्राध्यापक हैं )
भारत में हाल के हफ्तों में लोकतंत्र एवं सख्त आर्थिक सुधारों के बारे में एक बड़ी बहस ने जन्म लिया है। वित्त के क्षेत्र में सुधारों का मुख्य मार्ग लोकतंत्र की जड़ें गहरी होने से संबद्ध है। दुनिया की दूसरी जगहों, सुधारों के मामले में भारत के शुरुआती अनुभव और वित्तीय आर्थिक नीति के भावी सफर के बारे में भी ऐसा ही देखा गया है। लोकतंत्र का सार यानी सत्ता का प्रसार एवं कानून का शासन बाजार अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने के लिए अनुकूल हालात पैदा करते हैं और इसमें वित्त केंद्रीय अहमियत रखता है।
नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी अमिताभ कांत ने कथित तौर पर कहा है कि ‘सख्त’ सुधार कर पाना भारतीय संदर्भ में काफी मुश्किल है क्योंकि ‘हमारे यहां कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है’ लेकिन सरकार ने खनन, श्रम एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में ऐसे सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए ‘साहस’ एवं ‘संकल्प’ दिखाया है। इस बयान ने एक तूफान खड़ा कर दिया और तमाम आलोचक भारतीय लोकतंत्र के बचाव में आ खड़े हुए जिसके बाद अमिताभ कांत को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में लेख लिखकर यह सफाई देनी पड़ी कि उन्हें गलत समझा गया है।
चुनावों के माध्यम से सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की अवधारणा हमारे दिमाग में गहरी जमी हुई है लेकिन लोकतंत्र निर्वाचित शासक का फैसला करने वाले चुनाव से कहीं अधिक होता है। लोकतंत्र का सार सत्ता के फैलाव, राज्य की सत्ता के मनमाने इस्तेमाल के नियंत्रण और विधि के शासन की राह में राज्य सत्ता को समाहित करने में है। विधि के शासन के तहत निजी व्यक्ति एवं आर्थिक एजेंट इस पर सुरक्षित महसूस करते हैं कि राज्य की बाध्यकारी सत्ता को अप्रत्याशित, नियम-आधारित तरीके एवं निष्पक्ष ढंग से लागू किया जाएगा। इससे निर्माण फर्मों के निर्माण एवं व्यक्तिगत संपत्ति के सृजन में निवेश को बढ़ावा मिलता है। इस तरह लोकतंत्र के अभ्युदय और दशकों की मेहनत से अपनी फर्म खड़ा करने एवं अपनी संपत्ति को देश के भीतर ही बनाए रखने के लिए निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन के बीच काफी गहरा संबंध है।
बाजार अर्थव्यवस्था के सार यानी वित्त में ये अवधारणाएं पूरी शिद्दत से लागू होती हैं। हरेक वित्तीय प्रणाली में वित्तीय नियमन भी शामिल होता है। जब राज्य एवं नियामकीय शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता है तो नियामक अपने विवेक से निशाना तय करने लगते हैं। ऐसे हालात में निजी व्यक्ति पावर गेम में निवेश करने लगते हैं और वे राज्य सत्ता के इस्तेमाल को प्रभावित करने में जुट जाते हैं। निजी व्यक्तियों का ध्यान मुख्यत: राजनीतिक नियामकीय एवं अफसरशाही परिवेश को अपने अनुकूल ढालने पर लगा होता है जबकि अपने उपभोक्ताओं को समझने और संगठन चलाने के लिए कारगर तरीकों एवं तकनीक पर उनकी तवज्जो कम होती है।
इन वजहों से लोकतंत्र को मजबूत बनाने एवं बेहतर ढंग से संचालित एक वित्तीय प्रणाली के निर्माण के बीच मजबूत संबंध होता है। एक साझा कानूनी ढांचे में विधि-निर्माता या नियामक अधिक सिद्धांत-आधारित तरीके से काम करते हैं और राज्य उत्पादों या प्रक्रियाओं का ब्योरा नहीं तय करता है, राज्य विजेताओं को नहीं चुनता है, निजी व्यक्तियों का सूक्ष्म-प्रबंधन नदारद होता है एवं न्यायाधीशों को एक अनूठी स्थिति की परिकल्पना कर उसके अनुरूप कानून की व्याख्या करने की बड़ी भूमिका दी जाती है। ब्रॉउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राफेल ला पोर्टा एवं अन्य ने 1998 में ‘जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी’ में प्रकाशित अपने शोधपत्र में एक ऐसा विचार पेश किया था जिसके मुताबिक समान कानून ढांचा वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर ढंग से काम करता है। हाल में प्रकाशित एक लेख में लोकतंत्र का उच्च स्तर हासिल करने वाले देश से जुड़ी घटनाओं पर गौर करने के बाद यह पाया गया है कि लोकतंत्र का बढ़ा हुआ रूप संवद्र्धित वित्तीय विकास के लिए अच्छा रहा है। पीकिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यिपिंग हुआंग के 2010 में ‘वर्ल्ड डेवलपमेंट’ और डब्ल्यू गार्डेलू के 2016 में ‘जर्नल ऑफ फाइनैंशियल इकनॉमिक पॉलिसी’ में प्रकाशित शोध-पत्रों में इस संकल्पना की पुष्टि की गई। इस तरह अब हमें मालूम है कि अधिक लोकतंत्र वित्तीय विकास के नजरिये से अच्छा है।
वित्तीय क्षेत्र में विधायी सुधार के लिए आयोग एफएसएलआरसी का गठन 24 मार्च, 2011 को वित्त मंत्रालय ने किया था। भारतीय वित्तीय क्षेत्र के कानूनी एवं संस्थागत ढांचे की समीक्षा एवं उसे नए सिरे से लिखने के लिए यह आयोग बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी एन श्रीकृष्णा इस आयोग के प्रमुख बनाए गए थे और वित्त, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन एवं कानून से जुड़े जानकार इसके सदस्य बनाए गए थे। सचिव के अलावा इस आयोग के बाकी सारे सदस्य अकादमिक एवं शोध क्षेत्र और बाजार से जुड़े लोग थे। एफएसएलआरसी ने भारत के संविधान एवं भारतीय लोकतंत्र के भीतर वित्तीय नीति के प्रारूपों को चिह्नित किया। इसने कहा था कि एक लोकतंत्र में कानून का खाका तैयार करते समय निश्चित तौर पर सभी परिप्रेक्ष्यों को सुने जाने का मौका दिया जाना चाहिए।
यह रिपोर्ट एवं प्रारूप कानून सीधे तौर पर लोकतंत्र को सक्षम वित्तीय क्षेत्र के उद्देश्य की पूर्ति के लायक बनाने की बात करता है। आयोग की बुनियादी संकल्पना यह है कि ‘एक उदार लोकतंत्र में ‘शक्तियों का पृथक्करण’ सिद्धांत विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक गतिविधियों के बीच अलगाव को प्रोत्साहित करता है। वित्तीय नियामक इस मामले में अनूठे हैं कि ये तीनों तरह के काम एक ही एजेंसी संचालित करने लगती है। सत्ता का यह संकेंद्रण उत्तरदायित्व की मजबूत व्यवस्था के जरिये खत्म किए जाने की जरूरत है।’
नियामकों की स्वतंत्रतता के पक्ष में भी मजबूत तर्क दिए जाते हैं। स्वतंत्र नियामक कहीं अधिक कानूनी निश्चितता लेकर आएंगे। आयोग ने सुझाव दिया था कि नियामक की स्वतंत्रता की तलाश काम के दो पहलुओं को ध्यान में रखने पर खत्म होगी। एक तरफ स्वतंत्रतता को कानून में निहित किए जाने की जरूरत है और कानून में पूरे विस्तार से प्रक्रिया को तय कर ऐसा किया जाता है। दूसरी तरफ, आयोग ने एक प्रशासकीय राज्य से जुड़े खतरों और कानून का मसौदा बनाने एवं न्यायिक आदेश लिखने वाले अफसरों के बारे में कोई नियम न होने की तरफ भी ध्यान आकृष्ट किया था। लिहाजा स्वतंत्रता के साथ ही जवाबदेही तय करने वाली व्यवस्था की भी जरूरत है।
आयोग ने जवाबदेही तय करने के पांच तरीके सुझाए थे। नियामक के लिए निर्धारित प्रक्रिया का उल्लेख प्रस्तावित भारतीय वित्तीय संहिता (आईएफसी) में काफी विस्तार से लिखित रूप में किया जाना चाहिए। नियम-निर्माण की प्रक्रिया को आईएफसी के मसौदे में काफी विस्तार से दर्ज किया गया था। इसमें नियंत्रण एवं संतुलन प्रावधानों का भी उल्लेख है। अनिर्वाचित अधिकारियों को कानूनी मसौदा तैयार करने की शक्ति दिए जाने से एक अलग तरह का खतरा भी है। पर्यवेक्षण की व्यवस्थाएं विधि के शासन पर काफी तवज्जो की उपज रही हैं। इसके लिए रिपोर्ट दाखिल करने की सशक्त प्रणाली भी सुझाई गई थीं। आखिर में, नियामकों के सभी कार्यों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से गुजरने की व्यवस्था के तौर पर एक विशेष न्यायाधिकरण बनाने की बात कही गई और इस दौरान न्यायाधीश के तौर पर सिर्फ सेवानिवृत्त अफसरशाहों के ही काम करने की समस्या पर खास गौर किया गया।
समाधान की दिशा
संपादकीय
पिछले डेढ़ महीने से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के लापरवाही भरे रवैए पर सुप्रीम कोर्ट का नाराज होना स्वाभाविक है। सर्वोच्च अदालत सरकार से कहती रही है कि वह आंदोलनकारी किसानों से वार्ता कर मसले का उचित समाधान निकाले। लेकिन केंद्र की ओर से ऐसे प्रयास होते नहीं दिखे। अगर आठ दौर की वार्ताओं में भी सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाल पाने में समर्थ नहीं हुई जिससे आंदोलन खत्म कर किसान घरों को लौट जाएं तो यह व्यवस्था पर ही बड़ा प्रश्नचिह्न है। साफ है कि सरकार की मंशा आंदोलनकारी किसानों की बात सुनने और समस्या का हल निकालने की शायद नहीं है, बल्कि वह यह मान कर बैठ गई है कि एक न एक दिन किसान थक-हार कर लौट जाएंगे। वार्ताओं के लिए तारीखें देने के अलावा सरकार ने अपनी ओर से ऐसी कोई गंभीर और ठोस पहल नहीं की जिससे लगा हो कि वह इस समस्या का हल निकालना चाहती है। इसीलिए सोमवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ ने सख्त लहजे में सरकार को चेताया। अदालत ने साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इन कानूनों के अमल पर रोक भी लगा देगी। सर्वोच्च अदालत के रुख से इतनी उम्मीद तो बंधी है कि इस समस्या का अब कोई उचित और तार्किक समाधान निकलेगा।
नए कृषि कानूनों को लेकर शुरू से आवाजें उठती रही हैं। जिस हड़बड़ी में पहले अध्यादेश लाया गया और फिर कानून बना कर लागू कर दिए गए, उससे किसान तो क्या सभी के मन में संहेह पैदा हुए हैं। आखिर किसानों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नए कानून उनके हितों के खिलाफ हैं और कुछ उद्योग घरानों के हितों के लिए बनाए गए हैं? ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसा जरूर है जिसे किसान भी समझ रहे हैं और सरकार छिपा रही है। देश भर के लाखों किसान किसी राजनीतिक दल या विपक्ष के बहकावे में आकर इतना बड़ा और सख्त कदम उठा लें, ऐसा संभव नहीं है। किसानों की मांगों पर विचार के लिए सरकार अपने प्रतिनिधियों, कृषि मामलों के जानकार विपक्षी नेताओं, कृषि विशेषज्ञों और किसान संगठनों के नुमाइंदों की समिति ही बना देती और वह समिति किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करती तो समाधान की दिशा में बढ़ने का रास्ता निकलता। पर ऐसा नहीं हुआ। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने समझा है। अदालत भी यह देख रही है कि अगर किसान इस कदर उद्वेलित हैं तो जाहिर है कि नए कृषि कानूनों में कुछ तो ऐसा है जो उनके हितों के खिलाफ है। इसलिए अदालत ने कृषि कानूनों और किसानों के आंदोलन के संबंध में आदेश पारित करने की बात भी कही। साथ ही अदालत ने इस मामले पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीशों की एक समिति बनाने की बात भी कही है।
सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली वार्ता पंद्रह तारीख को होनी है। लेकिन अब तक का अनुभव यही बता रहा है कि इस वार्ता का भी कोई नतीजा निकलना, क्योंकि न तो सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने और न न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने का संकेत दे रही है। किसान संगठन इन दोनों मांगों के बिना आंदोलन खत्म नहीं करने वाले। फिर, कई राज्य भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और वे अपने यहां इन्हें लागू करने से साफ इंकार कर चुके हैं। इससे यह तो साफ है कि नए कृषि कानूनों को मौजूदा स्वरूप में अमल में लाने की सरकार की जिद कहीं ज्यादा बड़े टकराव को जन्म दे सकती है। ऐसे में अब उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय के प्रयासों से ही जगती है।
Date:12-01-21
नस्लीय दुराग्रह
संपादकीय
सभ्यता के विकास क्रम में समाज में कुछ स्वार्थी तत्त्वों की वजह से नस्ल, क्षेत्र, सामुदायिक पहचान आदि को लेकर अवांछित पूर्वाग्रहों के जन्म लेने और पलने-बढ़ने के बरक्स कालांतर में मनुष्य ने इनसे पार पाने की भी कोशिश की है। माना जाता है कि विकसित देशों में समाज और सत्ताओं ने इस तरह की धारणाओं को दूर करने के मसले पर काफी काम किया और काफी हद तक इसमें कामयाबी मिली है। लेकिन आज भी जब ऐसे पूर्वाग्रहों के साथ कुछ लोग दिख जाते हैं तो यह हैरानी और अफसोस की बात है। रविवार को सिडनी में आस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच में जिस तरह के हालात पैदा हुए, वह यह बताने के लिए काफी है कि विकसित कहे जाने वाले देशों में भी कुछ लोग नस्लवादी दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो सके हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की दुर्भावनाओं के साथ जीता है और उसे कुछ लोगों के बीच भी किसी स्तर की स्वीकार्यता प्राप्त है तो यह उस समूचे समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है।
गौरतलब है कि सिडनी टेस्ट में दूसरे और तीसरे दिन के खेल के दौरान नशे में धुत कुछ दर्शकों ने फील्डिंग करते जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर नस्लवादी टिप्पणियां कीं और लगातार गालियां भी दीं। यह दूसरे देश की धरती पर जाकर खेलने वाले किसी भी खिलाड़ी या व्यक्ति के लिए बेहद अपमानजनक और दुखद है। स्वाभाविक ही दोनों खिलाड़ियों ने प्रबंधन को इस बात की जानकारी दी और ऐसी टिप्पणियां करने वाले लोगों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तब क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने इन घटनाओं पर अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट किया कि हर तरह के भेदभाव को लेकर हमारी नीति साफ है; अगर आप नस्लवादी गालियां देते हैं तो आस्ट्रेलियाई क्रिकेट में आपकी कोई जरूरत नहीं है। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने एक कदम और आगे बढ़ कर मेजबान होने के नाते भारतीय क्रिकेट टीम से माफी मांगी। आस्ट्रेलियाई क्रिकेट की ओर से ऐसी सख्त प्रतिक्रिया इसलिए राहत की बात है कि वहां ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को सांस्थानिक स्तर पर कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। मगर सामाजिक स्तर पर यह न केवल आस्ट्रेलिया के लिए, बल्कि समूची दुनिया के लिए अफसोस और चिंता की बात है।
यों दुनिया के अलग-अलग देशों में आज भी नस्ल, क्षेत्र और समुदाय या जाति-समूहों को लेकर दुराग्रह या पूर्वाग्रहों से ग्रस्त धारणाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। खेल की दुनिया में भी गाहे-बगाहे ऐसे व्यवहार सामने आते रहे हैं, लेकिन अच्छा यह है कि इस पर औपचारिक रूप से उचित प्रतिक्रिया सामने आई और जरूरी कार्रवाई हुई है। करीब चार महीने पहले आस्ट्रेलिया के ही एक खिलाड़ी डेन क्रिश्चन ने कहा था कि उन्होंने अपने पूरे कॅरियर में नस्लवाद सहा है और अब उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी उनसे माफी मांगते हैं। दरअसल, नस्ल, जाति, समुदाय आदि को लेकर जिस तरह के पूर्वाग्रह देखे जाते हैं, वे व्यक्ति के सामाजिक प्रशिक्षण का हिस्सा रहे होते हैं और पैदा होने के बाद उनके भीतर जाने-अनजाने बैठा दिए जाते हैं। अफसोस यह है कि आलोचनात्मक विवेक के साथ इन मसलों पर विचार करने की कोशिश नहीं की जाती है। नतीजतन, कोई व्यक्ति कई बार निजी या फिर सार्वजनिक रूप से भी किसी अन्य नस्ल, जाति या समूह के लोगों को कमतर करने वाली या नफरत से भरी टिप्पणियां करके आहत करने की कोशिश करता है। जबकि समझने की बात यह है कि ऐसे पूर्वाग्रह या कुंठा पालने वाला कोई भी व्यक्ति सभ्य होने की कसौटी पर बहुत पिछड़ा होता है। इंसानों के भीतर इंसान के लिए समानता की संवेदना ही सभ्य होने की कसौटी है।
Date:12-01-21
दीर्घकालिक विकास की चुनौतियां
लालजी जायसवाल
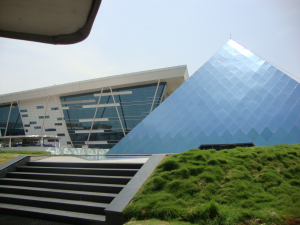
आज जब समूचा विश्व कोरोना महामारी से प्रभावित है, तब दीर्घकालिक विकास के लक्ष्यों की चर्चा चारों ओर हो रही है। 1908 में गांधीजी ने हमें इसी का मार्ग दिखाया था। अपने ‘हिंद स्वराज’ में उन्होंने भौतिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए हमारी खोज को देखते हुए मानव के भविष्य के लिए उत्पन्न खतरों को भी रेखांकित किया था। उन्होंने कहा था कि प्रकृति हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए नहीं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य का लालच विकास के सभी पहलुओं को विकृत करता जा रहा है और जीवनशैली से स्थायित्व की अवधारणा पृथक होती जा रही है। धारणीय जीवनशैली का अर्थ जीवन से उपभोक्तावाद को कम करना और सुख की जगह आनंद को तरजीह देना है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से सुखवादी और उपयोगितावादी होता है और ये दोनो ही प्रवृत्तियां दीर्घकालिक विकास के राह में बाधक है। आज मनुष्य के जीवन में उपभोक्तावाद का जहर इतना ज्यादा घुल चुका है कि वह प्रकृति के संसाधनों का अधिकतम दोहन कर लेना चाहता है, भले मानव जाति को इसके परिणाम कुछ भी क्यों न भुगतने पड़ें।
गौरतलब है कि उदारीकरण के बाद का युग आर्थिक संवृद्धि और प्रतिस्पर्धा का युग है, जिसमें केवल आर्थिक वृद्धि पर ही ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लेकिन ध्यातव्य है कि दीर्घकालिक विकास के दो प्रमुख शत्रु हैं, एक आर्थिक वृद्धि की होड़ और दूसरा- तेजी से बढ़ती जनसंख्या। इसी का परिणाम है कि आज दीर्घकालिक विकास की अवधारणा और प्रयास वाधित हो रहे हैं और इसी वजह से समय-समय पर मनुष्य को प्रकृति का कोपभाजन भी होना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति का दोहन करना मनुष्य अपना अधिकार मान बैठा है। प्रकृति में आज ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका मानव ने व्यापार न किया हो, फिर वह चाहे हवा हो अथवा पानी। उसका यही लालच आज समस्त मानव जाति के लिए काल बन कर अब तक विश्व भर में अठारह लाख लोगों की जान लील चुका है। मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन पिछली तीन सदियों में प्रकृति का दोहन इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज समूची धरती के लिए गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मनुष्य ने बस्तियां बसाने के लिए धरती से जंगलों का सफाया कर दिया। खेती तथा जमीन के लिए जंगलों में आग लगाई, प्राकृतिक संसाधनों का स्वामी बनने के लिए धरती को खोद डाला। जनसंख्या वृद्धि ने प्रदूषण फैलाया, पवन ऊर्जा के लिए पवन की गति को बाधित किया और अपनी आवश्यकता के लिए उद्योग-धंधे लगा कर प्रदूषण की समस्या खड़ी कर दी। आज दुनियाभर में नदियों का अस्तित्व गंभीर संकट में है। एक वक्त में जल का सबसे बड़ा स्रोत रहीं नदियां आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। बड़ी संख्या में नदियां प्रदूषण का संकट झेल रही हैं। प्रकृति के दोहन से मनुष्य को यह भरोसा हो गया था कि उसने प्रकृति को पूरी तरह पराजित कर दिया है। इन सभी प्रकृति विरोधी कार्यों से हम आर्थिक संबृद्धि तो दे सकते हैं लेकिन टिकाऊ विकास नहीं।
आज का दौर विशुद्ध उपभोक्तावाद का है, जिसकी वजह से मनुष्य अपना स्वत्व खोता चला जा रहा है और अर्थ केंद्रित हो गया है। हम पूंजीवाद को अपना सर्वस्व मान बैठे हैं, जिसमें प्रकृति के विनाश पर आर्थिक विकास की इमारत खड़ी होती है। ऐसे में यह दौर इस बात पर आत्मचिंतन करने का भी है कि आखिर हकीकत में पूंजीवाद ने हमें क्या प्रदान किया है? अगर वाकई गंभीरता से विचार करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि नतीजा यह निकलेगा कि वैश्वीकरण और इसकी आड़ में पनपी नई अर्थव्यवस्था की अवधारणा घातक ज्यादा साबित हुई है। वैश्वीकरण ने ओजोन परत क्षरण, भूमंडलीय ताप में वृद्धि, विलुप्त होते प्राकृतिक संसाधन, वातावरण प्रदूषण और छद्म आर्थिक वृद्धि व प्रतिस्पर्धा और मानव विनाशक विषाणुओं के अलावा और कुछ नहीं दिया है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना जैसी विनाशक महामारियों और आपदाओं ने मानव को चेतावनियां भी दी हैं। लेकिन लगता है हमने भी तक भी अपनी आंखें खोली नहीं हैं।
कोरोना महामारी से दुनिया में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। करोड़ों इसकी चपेट में हैं। लेकिन ऐसी आपदाएं दुनिया का स्वरूप भी बदल रही हैं। आज कुछ ही समय में भारत सहित कई देश डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। भारत जैसे देश ने संकट को अवसर में बदलते हुए आत्मनिर्भरता का रास्ता खोजने की कोशिश की। देश में कई विशेष उत्पाद सामने आए, जिनका हम पहले आयात करते थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मंद पड़ी अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना महामारी से ही आत्मनिर्भता का रास्ता अपनाने और जीवनशैली में बदलाव लाने की भी भरपूर सीख मिली है। लेकिन कहीं हम इस सबक को आने वाले समय में भुला न बैठें। यह भी सत्य है कि अगर मनुष्य इस महामारी से हासिल सबक को अपना लेता है तो समूचा जीवन एक आदर्शतम रूप में होगा और विकास भी आर्थिक संवृद्धि मात्र न होकर सतत और दीर्घकालिक होगा। ऐसा कर हम पुन: अपने आदर्श जीवन की ओर लौट सकते हैं।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि एक महामारी भी हमें दीर्घकालिक विकास के प्रति सचेत कर सकती है और उसका रास्ता दिखा सकती है। इसलिए अब हमें विकास के उन तरीकों को त्यागने में देर नहीं करनी चाहिए जो जीवन के लिए संकट का कारण बन रहे हैं। जैसे हमें प्लास्टिक उपयोग से बचना होगा और पर्यावरण को बचाना होगा। डेनिस डोनेला (डेनमार्क) ने अपने शोध पत्र में कहा था कि अगर एक वृक्ष काटा जाए तो एक वृक्ष लगाना साम्यावस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर हम एक वृक्ष काटते है और बदले में पांच पौधे भी लगाते हैं, पर उसकी नियमित देखभाल नहीं करते तो यह पर्यावरण विदोहन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अगर मनुष्य जीवन में धारणीय शैली को अपना ले तो विकास स्वयं ही धारणीय बनता चला जायेगा। स्पष्ट है कि मनुष्य पर्यावरणीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा कर अपने आयुष्मान होने की कल्पना नहीं कर सकता। हमें नही भूलना चाहिए कि धारणीय विकास एक विशाल यज्ञ की तरह है, जिसमें समाज के हर वर्ग को अपनी आहुतियां डालनी होंगी। इस क्षेत्र के अगुआ देशों के अनुभवों से ज्ञान लेकर अगर हम सरकार और समाज की साझेदारी करने में सफल हो गए, तो धरती पर जीवन बचाने में कामयाब हो सकेंगे।
समाधान की ओर
संपादकीय
तीन कृषि कानूनों को लेकर चल रहा विवाद सुप्रीम कोर्ट में समाधान की दिशा में बढ़ता लग रहा है, तो यह सुखद और स्वागतयोग्य है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ समाधान के लिए बहुत लालायित और दृढ़ दिखी है, जिससे लगता है, जल्द ही कोई समाधान निकलेगा। सोमवार को सुनवाई के दौरान उभरे तीन-चार संकेत बहुत स्पष्ट हैं। पहला संकेत तो यही है कि सर्वोच्च अदालत नए कृषि कानूनों पर कुछ समय के लिए रोक लगा सकती है। हालांकि, रोक लगाने जैसी किसी घोषणा की उम्मीद उसे केंद्र सरकार से भी है। दूसरा संकेत, केंद्र सरकार विवाद सुलझाने के लिए और वक्त चाहती है, लेकिन अदालत अब इसके लिए बहुत सहमत नहीं लगती। संकेत यह है कि अदालत एक समिति का गठन कर सकती है, जो कृषि कानूनों की समीक्षा करेगी और उसके नतीजों के आधार पर सर्वोच्च अदालत को फैसला लेने में सुविधा होगी। वैसे समिति के गठन का सुझाव पहले भी आ चुका है, जिसे किसान ठुकरा चुके हैं। कोई आश्चर्य नहीं, किसानों ने सोमवार को सर्वोच्च अदालत के रुख की तारीफ की, लेकिन समिति गठन के उसके सुझाव पर असहमति जताई। समिति के गठन, कृषि कानूनों की समीक्षा और अंतिम रिपोर्ट में काफी समय लग सकता है। अत: शीर्ष अदालत यदि समिति का गठन करे, तो फिर उसकी रिपोर्ट के लिए भी एक न्यूनतम समय-सीमा तय होनी चाहिए।
सर्वोच्च अदालत ने उचित ही यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान-सम्मत जो भी होगा, वह अवश्य करेगी। अदालत का साहसिक रुख दोनों पक्षों को समाधान के लिए प्रेरित करे, तो स्वाभाविक है। ऐसे विवादों को सुलझाने में जितनी साफगोई रहे, उतना ही अच्छा है। जो संविधान की रोशनी में उचित या व्यावहारिक है, उसी दिशा में बढ़ना आज समय की मांग है।
अदालत की ओर से सामने आया तीसरा संकेत यह है कि सरकार कृषि कानूनों के फायदे के प्रति अदालत को सहमत या आश्वस्त नहीं कर सकी है। सरकार अगर आश्वस्त कर देती, तो अदालत को समिति गठन की जरूरत महसूस नहीं होती। सबसे जरूरी है, किसानों का आश्वस्त होना। अभी भी सरकार के पास मौका है, किसानों के साथ अगली बातचीत में कृषि कानूनों के ठोस फायदों के साथ किसानों को आश्वस्त करने की जरूरत है। जो समिति बनेगी, वह भी यही काम करेगी। किसानों व सरकार को इस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। किसानों को समिति से इनकार का हठ छोड़ देना चाहिए। बेहतर यही होगा कि किसान यह समझाने का प्रयास करें कि ये कृषि कानून किस तरह उनके प्रतिकूल हैं। सरकार और किसानों को अंतत: अपने-अपने तथ्य-तर्क के साथ बैठना होगा। अब यह इन दोनों को तय करना है कि समिति स्वयं किसानों व सरकार की होगी या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित। लोग जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। प्रतिकूल मौसम में लंबे समय तक ऐसे आंदोलन का चलना किसी के लिए भी सही नहीं है। बुजुर्ग, महिला और बच्चे जान जोखिम में डालकर सड़कों पर बैठे हैं, कड़ाके की सर्दी भी है और असमय बारिश ने भी बेहाल कर रखा है। लोगों को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। अगर यह विवाद गणतंत्र दिवस से पहले सुलझ जाए, तो यह देश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।
Date:12-01-21
सिर्फ शब्द न रह जाए संविधान
विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी
जमशेदपुर कई अर्थों में बड़ा दिलचस्प शहर है। यहां 1907 में टाटा औद्योगिक घराने की नींव रखने वाले जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा ने इलाके के पहले बडे़ कारखाने टिस्को की स्थापना के साथ ही भविष्य के एक बड़े शहर की शुरुआत भी की थी। आज अपनी सुदृढ़ नागरिक सुविधाओं, फुटबॉल और शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त यह शहर मुझे इसके नागरिकों की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहसों में सक्रिय भागीदारी और गहरी समझ के लिए उल्लेखनीय लगता है। इस शहर की मेरी चौथी यात्रा एक ऐसे कार्यक्रम के सिलसिले में थी, जिसका विषय शुरू में तो मुझे घिसा-पिटा लगा, पर वहां जाकर शहरियों की भागीदारी और जुड़ाव देखकर समझ में आया कि हाशिए पर अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, दलितों या औरतों के लिए ऐसे विमर्श क्या अर्थ रखते हैं? विषय भारतीय संविधान और उसके चलते देश की अखंडता या संप्रभुता को बचाने से जुड़ा था। आयोजक संस्था का नाम भी ‘देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान’ है। विभिन्न राजनीतिक दलों और स्वयंसेवी संगठनों से जुडे़ ये लोग संविधान को लेकर कितने चिंतित हैं, इसे इनके पिछले कुछ वर्षों के कार्यक्रमों की सूची देखकर समझा जा सकता है।
कुछ ही दिनों में हम 72वां गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं। हाल-फिलहाल बहुत कुछ ऐसा घटा है, जिसके चलते नागरिकों को स्मरण कराना जरूरी है कि संविधान की हिफाजत की शपथ लेते रहना सिर्फ औपचारिकता नहीं है। आजादी के फौरन बाद मुसलमानों की एक पस्त भीड़ के सामने बोलते हुए मौलाना आजाद ने कहा था कि उन्हें तब तक अपनी हिफाजत की चिंता नहीं करनी चाहिए, जब तक 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान सुरक्षित है। अब तो देश के दूसरे हाशिए के समुदायों को भी समझ में आ गया है कि अगर संविधान नहीं बचा, तो उनके एक सभ्य मनुष्य के रूप में जीने की संभावना भी नहीं बचेगी। इस संविधान के बनने और उसके जनता द्वारा स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया को बार-बार याद किए जाने की जरूरत है।
1947 से 1949 के बीच नई दिल्ली की संविधान सभा में जो कुछ घट रहा था, वह किसी शून्य से नहीं उपजा था। यह असाधारण जरूर था, पर अप्रत्याशित तो बिल्कुल नहीं कि रक्तरंजित बंटवारे के बीच काफी लोगों ने मान लिया था कि हिंदू और मुसलमान, दो अलग राष्ट्र हैं, इसलिए साथ नहीं रह सकते। तब संविधान सभा ने देश को ऐसा संविधान दिया, जो एक उदार और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की परिकल्पना करता है। यह अप्रत्याशित इसलिए नहीं कि देश की आजादी की लड़ाई जिन मूल्यों से परिचालित हो रही थी, वे आधुनिकता और धर्मनिरपेक्षता की ही उपज थे। अस्पृश्यता या स्त्री-पुरुष समानता जैसे प्रश्नों पर संविधान सभा की दृष्टि एक आधुनिक दृष्टि थी और इसके चलते भारतीय समाज में दूरगामी परिवर्तन होने जा रहे थे। इसी तरह, एक करोड़ से अधिक लोगों के विस्थापन और विकट मार-काट के बीच भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अर्जित एकता की भावना ने ही इस धर्मनिरपेक्ष संविधान को संभव बनाया।
यह संविधान 26 नवंबर, 1949 को बन तो गया, पर इसे बनाने वाली सभा ही जनता से सीधे नहीं चुनी गई थी और इसकी वैधता के लिए जरूरी था कि इस पर जन-स्वीकृति की मोहर लगवाई जाए। इस जिम्मेदारी को निभाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ 1952 के पहले आम चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। चुनाव के पहले 1951 में उन्होंने देश भर में घूम-घूमकर 300 सभाएं कीं। जालंधर से शुरू हुई उस शृंखला में उनका एक ही एजेंडा था, लोगों को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए तैयार करना। हर सभा में वह इस सवाल से अपना कार्यक्रम शुरू करते, देश बंटवारे के साथ आजाद हुआ है, हमारे बगल में एक धर्माधारित इस्लामी हुकूमत कायम हो गई है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी एक हिंदू राज बना लेना चाहिए? इन सवालों के जवाब वह खुद अगले डेढ़ घंटे तक आसान हिन्दुस्तानी में देते। वह लगभग अशिक्षित श्रोताओं को अपने तर्कों से कायल करके ही भाषण समाप्त करते कि कैसे देश की एकता, अखंडता और तरक्की के लिए एक धर्मनिरपेक्ष भारत जरूरी है। समय ने उन्हें सही साबित किया। मजहब के नाम पर बना पाकिस्तान 25 वर्षों में ही टूट गया और तमाम हिचकोलों के बावजूद भारत एक मजबूत राह पर आगे बढ़ रहा है। जालंधर को पहले सभा-स्थल के रूप में चुनना नेहरू की आगे बढ़कर चुनौती स्वीकार करने की प्रवृत्ति का ही परिचायक था। गौर कीजिए, जालंधर की उनकी सभा के अधिसंख्य श्रोता वे हिंदू और सिख थे, जो कुछ ही दिनों पहले बने पाकिस्तान से अपने प्रियजनों और जीवन भर की जमा-पूंजी गंवाकर वहां पहुंचे थे। नेहरू जानते थे कि अगर इन हिंसा पीड़ितों को वह समझा सके कि धार्मिक कट्टरता बुरी चीज है, तो बाकी देश में उनका काम आसान हो जाएगा। यही हुआ भी, चुनावी नतीजों ने एक धर्मनिरपेक्ष संविधान को वैधता प्रदान कर दी।
जमशेदपुर के कार्यक्रम में न्यायविद फैजान मुस्तफा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। एक अच्छे संविधान के बावजूद अमेरिका में ट्रंप के उकसावे पर भीड़ संसद पर चढ़ दौड़ी, इस स्थिति में सारी सदिच्छाओं का क्या होगा? वहां कम से कम संस्थाओं में इतना दम तो है कि प्रारंभिक झटके के बाद उन्होंने अपने राष्ट्रपति का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। क्या हमारी संस्थाएं इतनी मजबूत हैं? लोकतंत्र में जरूरी है कि विवाद या तो बातचीत से हल हों या फिर संविधान के दायरे में न्यायिक समीक्षा द्वारा, पर हाल का किसान आंदोलन इस मामले में निराशाजनक है कि सरकार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजने की बात की। संविधान की रोशनी में सरकार को खुद आगे बढ़कर समाधान की तलाश करनी चाहिए।
हमारे तंत्र पर ऐसे खतरे तब तक मंडराते रहेंगे, जब तक हम संविधान में शामिल धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता या कानून के सामने सबकी बराबरी जैसे मूल्यों को अपनी जीवन पद्धति का अंग नहीं बनाएंगे। संविधान में दर्ज शब्द कितने खोखले हो सकते हैं, यह हमसे बेहतर कौन जान सकता है?
