
10-07-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:10-07-23
Date:10-07-23
Numbers Game
Official data quality is worsening. GOI should empower the National Statistical Commission.
TOI Editorials
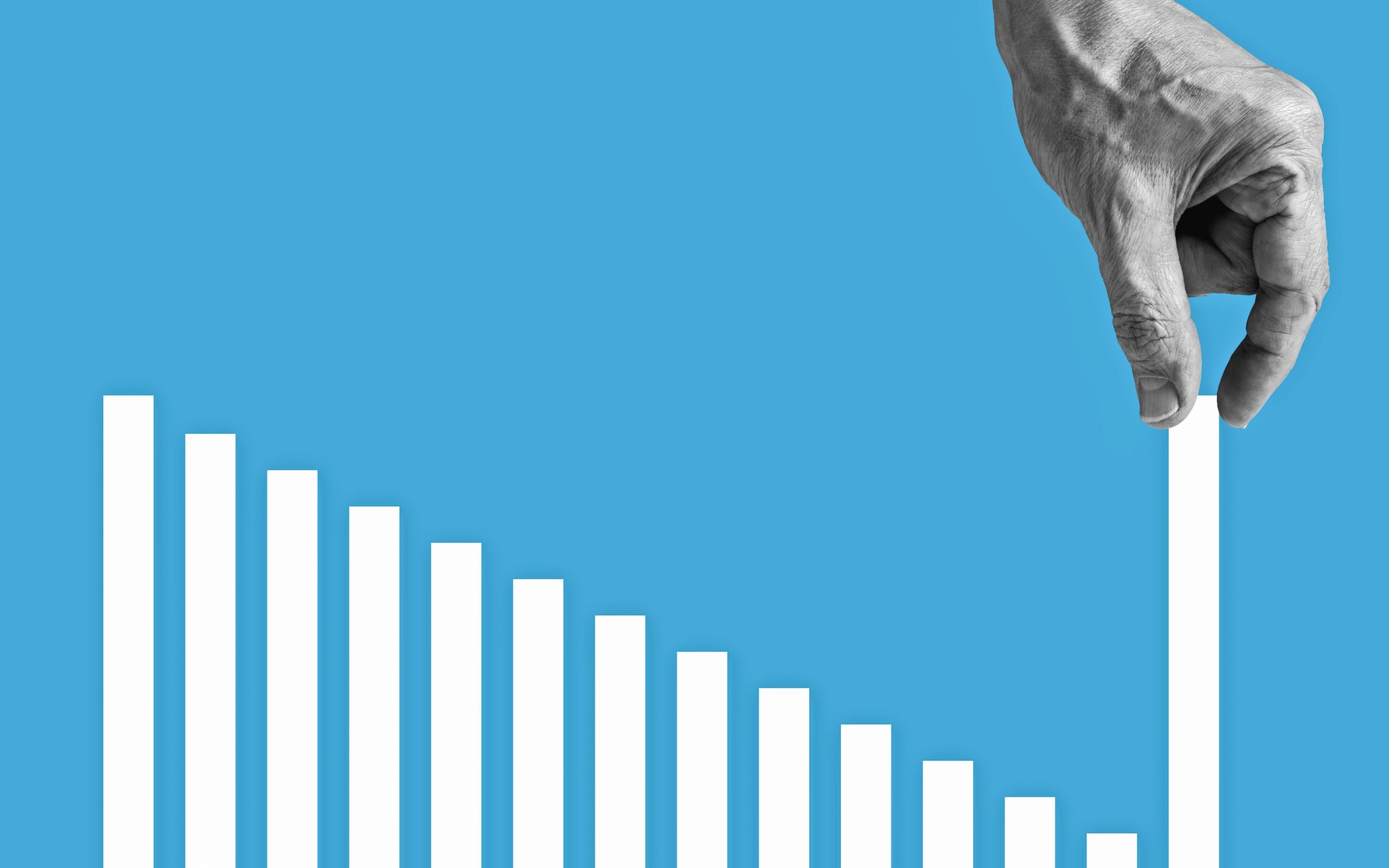
In the last four months, three members of the PM’s economic advisory council have independently expressed concern about the quality of official statistics. The critique of the statistical system is now coming from within the establishment. It’s pertinent because it provides a sense of the challenges of economic policymaking. In the absence of reliable data, policymaking is akin to flying blind.
India has built an impressive structure to capture administrative data by governments that can then be fed into the statistical system. However, this mode of data collection needs to be complemented by the official statistical system generating primary data through surveys to fill the gaps. It’s the survey data, where our statistical system was a pioneer in the 1950s, that has proved to be problematic. Unless this challenge is addressed urgently, we run the risk of opting for wrong policies not because the future is unknowable, but because past data is unreliable.
There are two main problems today with the statistical system.
One, timetables to generate primary data are not followed rigorously. The most serious of these is the indefinite delay in the Census. It’s unprecedented and has left a big hole in the data system. There are also delays in the consumer expenditure survey and the economic census. Among critical measures affected by these delays are the monthly inflation readings and the GDP data. Two, there are complaints from the users about the quality of data. Put together, delays and doubts about quality have left India data poor. None of these problems is of recent origin. They have been building up over time.
A National Statistical Commission was constituted in 2006 as an apex body for statistical activities and to set standards. It was meant to be empowered by legislation. Seventeen years later, the legislation hasn’t been passed and the official statistical system at both Centre and states is in trouble. Among the in-house recommendations to empower NSC was one that wanted its members picked through a committee represented by a wide spectrum of parliamentarians. It’s essential to insulate the statistical system from charges of political bias. A mechanism to ensure financial autonomy was also suggested. These suggestions remain valid. An upgrade to the statistical system has to be overseen by a technically equipped body that has statutory powers. Reliable data is an essential need.
Date:10-07-23
Why They Leave
Kejriwal says students should ‘work for the country’. What’s important to the young is what works in the country.
TOI Editorials

That involves many things, including improving the supply of quality education and a more enabling economic environment. That this can be done has been proved in part by Kejriwal’s government itself, which substantially improved the quality of education in Delhi’s government schools. And that an altered cost-benefit equation reduces the flow of students going out is evident from one of the best education institutes in the country – as a TOI story on Sunday showed, the number of IIT Bombay computer science graduates who leave for the US has dropped sharply, because many are now becoming tech entrepreneurs in India’s vibrant startup ecosystem.
Separately, and Kejriwal must know this already, Indians abroad, whether students or professionals or entrepreneurs, are an asset for India. The diaspora improves the optics for India, it speaks for India, and it’s a source of investment and ideas. If any of those Delhi government school students Kejriwal spoke to pursue further education abroad, they will be part of that beneficial collective. “Work for the country,” seems like a noble thought, a good advice, but it lacks any substantive meaning for young people making life decisions. What’s important for them is what works in the country.
Restoring the World Trade Organization’s crown jewel
With the United States now hostile towards the WTO’s dispute settlement system, the resurrection of the mechanism by 2024 could face trouble.
Prabhash Ranjan teaches at the Faculty of Legal Studies, South Asian University.
In June 2022, the member-countries of the World Trade Organization (WTO) managed to hammer out a face-saving deal — India played a vital role — at the Geneva ministerial conference, thereby keeping faith in trade multilateralism alive. An important part was resurrecting the WTO’s dispute settlement system (DSS), also called WTO’s ‘crown jewel’, by 2024. Since 2019, the WTO’s two-tiered DSS remains paralysed. The appellate body, which is the second tier of the WTO’s DSS that hears appeals from WTO panels, is non-functional because the United States, single-handedly, has blocked the appointment of its members. The appellate body, from 1995-2019, has upheld the international rule of law by holding powerful countries such as the U.S. and the European Union accountable for international law breaches. However, the appellate body has become a victim of its success. Its one-time supporter, the U.S., has become its most acerbic critic. Now, the clock is ticking, and from the information publicly available, it looks unlikely that the DSS will be in the pink by 2024.
The ‘precedent’ problem
The U.S. reproaches the appellate body for judicial overreach and exceeding its assigned institutional mandate. Thus it argues that till the time the appellate body’s role is defined precisely, it cannot be resurrected. One major problem that the U.S. identifies is that the appellate body, contrary to the text of the WTO’s dispute settlement understanding (DSU), has been creating binding precedents through its decisions.
It is well-established that there is no rule of stare decisis — i.e., no rule of precedent in international law. The WTO’s DSU also makes this clear in Article 3.2 by stating that the appellate body rulings can neither add nor diminish the rights and obligations of WTO member-countries. However, the same Article also says: “The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing security and predictability to the multilateral trading system.” Thus, it is incumbent on the appellate body to ensure that there is consistency in the interpretation and application of the WTO agreements without creating a binding precedent. This requires striking a fine balance — precisely what the appellate body has tried to do. It has encouraged the WTO panels to rely on previous interpretations especially where the issues are the same. Simultaneously, the appellate body has clarified that a departure can be made from the previous rulings and reasoning if there are “cogent reasons”. The argument that this means that the appellate body is following a system of precedent in the sense it is followed in the common law system is tantamount to vastly overstating the case, as James Bacchus and Simon Lester argue.
Moreover, the appellate body is not the only international court that follows its previous decisions. Other international courts such as the International Court of Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea also follow past decisions unless there are valid reasons not to do so. At any rate, it has been proposed that the WTO member-countries can adopt a statement that the appellate body rulings do not create precedents. However, it will not satisfy the U.S.
De-judicialisation of trade multilateralism
The larger game plan of the U.S. seems to be the de-judicialisation of trade multilateralism as we know it. The WTO was created in a world that was resplendent with the neoliberal consensus that emerged after the Cold War and the collapse of communism. Ernst-Ulrich Petersmann, an international economic lawyer, argued that in a neoliberal economic system, the ‘invisible hand’ of market competition should be complemented by the ‘visible hand’ of the law. The WTO became this ‘visible hand’ of the law to regulate global trade. This period saw not only the legalisation of international relations (states accepting precise international law standards to judge their behaviour and delegating this power to judge to international courts) but also its judicialisation (the expansion of international courts and tribunals that dominate decision-making in place of national actors). This, arguably, erodes the sovereignty of nations as they lose control over critical decision-making. De-judicialisation, as Daniel Abebe and Tom Ginsburg define it, is the reverse phenomenon where countries weaken international courts to take back decision-making power. Given the emerging geo-economic challenges posed by a rising China, the U.S. wants to exercise full power over its trade policies, throwing off the shackles of the appellate body’s judicial review. This de-judicialisation should not be confused with exerting political oversight over the appellate body to improve its working. While Washington has identified multiple problems with the DSS, it has seldom offered constructive suggestions.
On voting
It is a fool’s errand to negotiate with the U.S. to put the appellate body back on track. One option that other countries have, as Henry Gao argues, is to elect the appellate body members by resorting to voting at the WTO’s General Council meeting. But this will antagonise the U.S. Are countries willing to go down that road?
नए भारत को चाहिए नया प्रशासनिक ढांचा
विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा, ( देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में अपर निजी सचिव-अनुसंधान हैं )
ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर का भग्नावशेष बना भारत का प्रशासनिक ढांचा देश की तेजी से बढ़ती आबादी और विविधतापूर्ण एवं समयानुकूल आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम नहीं दिख रहा। कालातीत हो चुका यह ढांचा देश की प्रगति को अवरुद्ध कर सक्षम एवं प्रभावी जन सेवाएं प्रदान करने में नाकाम हो रहा है। इसलिए देश के बेहतर भविष्य के लिए प्रशासनिक सुधार कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य हो गए हैं। कई विद्वान एवं विश्लेषक समय-समय पर इनकी आवश्यकता बताते रहे हैं। जैसे कि औपनिवेशिक प्रशासनिक अमले की विरासत से उपजी चुनौतियों को लेकर प्रतिष्ठित राजनीति विज्ञानी एवं संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल आस्टिन ने दर्शाया था कि इस प्रणाली में लचीलेपन का अभाव है और यह नागरिकों के अनुसार स्वयं को ढालने और आकार ले रहे सामाजिक परिवर्तनों से ताल मिलाने में अक्षम है। संविधान शिल्पी और सामाजिक न्याय के प्रवर्तक डा. बीआर आंबेडकर ने भी समतामूलक समाज के निर्माण में प्रशासनिक सुधारों की महत्ता को रेखांकित किया था। उनका कहना था कि औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों वाला प्रशासनिक ढांचा देश के समक्ष विद्यमान सामाजिक-आर्थिक विषमताओं के समाधान में प्रभावी रूप से उपयोगी नहीं हो सकता।
अब सक्षमता, पारदर्शिता, जवाबदेही और तत्परता जैसे पहलुओं के आधार पर प्रशासनिक ढांचे को नए सिरे से खड़ा करने के लिए सुधारों की मांग जोर पकड़ रही है। इसका उद्देश्य ऐसी नौकरशाही का निर्माण करना है जो लोगों की सेवा करे, विकास को गति दे और सभी नागरिकों तक समान अवसर सुनिश्चित कर सके। इसमें भ्रष्टाचार पर प्रहार, अक्षमताओं से मुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और तकनीकी का लाभ उठाने पर जोर है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में नागरिकों की आकांक्षा पूर्ति की दिशा में ऐसे सुधारों के लिए ढांचागत बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में, प्रशासनिक ढांचे पर चढ़ी औपनिवेशिक खुमारी उतारकर एक ऐसे प्रशासनिक तंत्र की राह प्रशस्त करना आवश्यक हो चला है जो विशुद्ध भारतीय चरित्र एवं मूल्यों से ओतप्रोत हो। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में प्रशासनिक सुधार महज आवश्यकता न होकर राष्ट्र की प्रगति, विस्तार एवं संसाधनों की उचित साझेदारी के लिए एक पूर्वनिर्धारित शर्त बन गई है।
अक्षमता और भ्रष्टाचार प्रभावी लोक सेवाओं की राह में बड़े अवरोधक हैं। भ्रष्टाचार लोक सेवाओं की गुणवत्ता घटाने के साथ ही शासन में जनता के भरोसे को भी घटाता है। इसलिए सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में भ्रष्टाचार से निपटना बड़ी चुनौती है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के खाते में सीधे रकम पहुंचाकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ी पहल की है। इससे सरकारी संसाधनों का रिसाव रुका है। हालांकि, राष्ट्रजीवन के कुछ अन्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का दंश अभी भी लोगों को चुभ रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस का मामला ही ले लीजिए। इसमें कई बार अपात्र लोगों को भी लाइसेंस मिल जाता है। ऐसे लोग गाड़ी चलाते हुए न केवल खुद के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी जोखिम बन जाते हैं। वहीं, पात्र लोगों को भी जेब ढीली करनी पड़ जाती है। दोनों स्थितियों के लिए भ्रष्टाचार जिम्मेदार है, जिस पर लगाम लगानी होगी और यह सुधारों के बिना संभव नहीं होगा।
प्रशासनिक सुधारों के पीछे मंशा केवल एक ढांचे का कायाकल्प करना ही नहीं, बल्कि लोक सेवाओं को और बेहतर बनाने के साथ ही नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं की कसौटी पर खरा उतरने की भी है। इस दिशा में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस बल, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में सुधार भी करने होंगे। इसमें पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी अहम पहलू हैं, क्योंकि किसी समाज के जागरूक एवं सक्रिय बनते जाने पर इन्हें लेकर मांग और मुखर होती जाती है। जनस्तर पर आकार ले रहा परिवर्तन भी प्रशासनिक सुधारों की मांग को गति दे रहा है। ऐसे सुधारों में तकनीक को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं आधुनिक एवं सुसंगत बनेंगी।
भारतीय प्रशासनिक ढांचे में जिला स्तरीय इकाई बहुत महत्व रखती है, पर कई कारणों से वे खासी अक्षम बनी हुई हैं। इसमें शक्ति का अति-केंद्रीकरण प्रमुख है, जिसमें ताकत राज्य स्तर पर केंद्रित रहती है। इसमें जिला प्रशासन के पास निर्णय लेने की गुंजाइश सीमित हो जाती है। जबकि कई समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सकते हैं, लेकिन उनके पास इस दिशा में आगे बढ़ने का अधिकार नहीं होता। रही सही कसर वित्तीय से लेकर मानव संसाधनों के अभाव से पूरी हो जाती है। इस कारण आवश्यक सेवाओं और परियोजनाओं को सिरे चढ़ाना आसान नहीं रह जाता। लालफीताशाही और हद से ज्यादा विस्तार वाली प्रशासनिक प्रक्रियाएं बहुत भारी पड़ती हैं। इससे नागरिकों में असंतुष्टि एवं आक्रोश बढ़ता है। जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच लचर तालमेल से भी काम में दोहराव और संसाधनों की बर्बादी होती है। कई जिलों में ई-गवर्नेंस को अपना लिया गया है तो तमाम अभी भी पारंपरिक कागजी तौर-तरीकों से संचालित हो रहे हैं, जिनसे सेवाओं के स्तर और प्रभावोत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे भी बदतर बात यही है कि जिले में सक्रिय प्रशासनिक अमले के पास अक्सर आवश्यक प्रशिक्षण एवं कौशल का भी अभाव होता है, जिससे अक्षम प्रबंधन और गलत निर्णय की स्थिति उत्पन्न होती है। वास्तव में जिला अधिकारी संस्था की भी नए सिरे से संकल्पना की जानी चाहिए। अभी कई मामलों में जिला अधिकारियों को 100 से अधिक जिला स्तरीय समितियों की अध्यक्षता करनी पड़ती है। यह बहुत ज्यादा है। इसीलिए व्यापक प्रशासनिक सुधार आवश्यक हो गए हैं। चूंकि देश में प्रशासनिक सुधार के मोर्चे पर स्वतंत्रता के बाद से अब तक कई आयोग और समितियां बन चुकी हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए हैं। इस कारण भविष्य में होने वाले प्रशासनिक सुधार दिखावटी या मामूली स्तर के न होकर ऊंची छलांग लगाने वाले होने चाहिए, जो नए भारत की आकांक्षाओं के साथ बखूबी कदमताल कर प्रशासनिक ढांचे को सक्षम बनाते हुए पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी सुनिश्चित कर सकें।
Date:10-07-23
इतिहास को राजनीति से बचाएं
जगमोहन सिंह राजपूत, ( लेखक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव एवं पंथक समरसता के क्षेत्र में कार्यरत हैं )
स्कूली बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक केवल अध्ययनशील, विचारवान, अनुभवी और जीवन तथा परिवर्तन के प्रति वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति द्वारा ही लिखी जानी चाहिए। राजनीति या राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले लोग भले ही शैक्षिक पदों पर विद्यमान हों, उच्च श्रेणी का शोध कर रहे हों, पाठ्यपुस्तक लिखने से उनका दूर रहना ही राष्ट्रहित में होगा। लोकतंत्र में पाठ्यपुस्तक लेखकों का ही नहीं, जनप्रतिनिधियों का भी यह शाश्वत उत्तरदायित्व है कि बच्चों को किसी राजनीतिक अवधारणा के प्रति प्रेरित कराने का प्रयास न किया जाए, उन्हें केवल वस्तुनिष्ठ जानकारी प्रदान की जाए। हालांकि ऐसा वह व्यक्ति कतई नहीं कर सकता है, जो राजनीतिक दलों से संबंद्ध हो या रहा हो, दल बदलता रहा हो और इसके बाद भी नैतिकता की बात करता हो। पाठ्यपुस्तकों को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी पर जब राजनीति से प्रेरित आक्रमण होते हैं, तब सत्य तो यही उभरता है कि यह स्वार्थ-प्रेरित हैं और एक राष्ट्रीय संस्था की साख पर बट्टा लगाने के कुत्सित प्रयास हैं।
एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और स्कूली शिक्षा के विभिन्न आयामों पर शोध के क्षेत्र में राष्ट्र की अग्रणी संस्था है। इसका पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और उनमें सुधार का छह दशकों से अधिक का अनुभव है। इसकी अपनी साख और स्वीकार्यता है। इस साख के बनने में अनेकानेक विद्वानों के साथ ही उन प्राध्यापकों, विद्वानों और शोधकर्ताओं का भी बड़ा योगदान रहा, जिन्हें वामपंथी-मार्क्सवादी खेमे का माना जाता रहा है। इनका शिक्षा संस्थानों और उनके सभी कार्यकलापों और नियुक्तियों तक पर पर चार दशक से अधिक समय तक पूर्ण वर्चस्व रहा है। केवल वर्ष 1998 से 2004 और वर्ष 2014 से वर्तमान दौर में ही यह वर्ग इस विशेषाधिकार से वंचित रहा। इससे उनमें घनघोर आक्रोश, ईर्ष्या और आक्रामकता का उभरना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में भी जो लोग सत्ता या संस्थानों पर आधिपत्य पा जाते हैं वे अक्सर यह मान लेते हैं कि वहां बने रहने का अधिकार केवल उनका या उनके परिवारजनों का ही है। जिन लेखकों की पुस्तकें दो-तीन दशक से देश के स्कूलों में चल रही थीं, वे इस संभावना से ही उत्तेजित हो गए कि कोई अन्य लोग उनका स्थान ले सकते हैं या पाठ्यपुस्तकें बनाने का दुस्साहस कर सकते हैं। आज एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से कुछ अंश हटाने को लेकर कुछ विद्वानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अवार्ड-वापसी की जानी-पहचानी तर्ज पर पर कहा है कि उनके नाम इन पाठ्यपुस्तकों से हटा दिए जाएं! संभव है ये लोग वह मानदेय भी वापस कर दें, जो एनसीईआरटी से प्राप्त किया होगा। एनसीईआरटी को इनका अनुरोध तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए।
इस समय जो हो रहा है उसमें नया कुछ नहीं है, वह तो अपेक्षित ही था। वर्ष 1999 से 2004 के मध्य भी एनसीईआरटी के विरुद्ध एक राजनीति-प्रेरित अभियान चलाया गया था। पुस्तकों में बदलाव से पहले पाठ्यचर्या (करिकुलम) बनाना, फिर पाठ्यक्रम (सिलेबस) और फिर पुस्तक निर्माण का क्रम अपनाया जाता है। 28 सितंबर, 2001 को दिल्ली विधानसभा में एनसीईआरटी के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया गया कि उसकी नई पुस्तक में गुरु तेग बहादुर साहिब के संबंध में जो अत्यंत अपमानजनक तथा आधारहीन वर्णन है और उसे तुरंत हटा दिया जाए। यह किताब नई नहीं थी, दशकों पुरानी पुस्तक का ही पुनर्मुद्रण था, लेकिन एनसीईआरटी ने इस पर ध्यान दिया, अनेक इतिहासकारों से चर्चा की और उस आधार पर सीबीएसई से कुछ अंश न पढ़ाए जाने का अनुरोध किया। आलोचना किस कदर आंख मूंदकर की जाती है, यह उसका ही एक उदाहरण है।
राजनीति और विचारधारा से जकड़ा हुआ पाठ्यपुस्तक लेखन भावी पीढ़ियों के साथ कितना अन्याय करता है इसे समझने के लिए एनसीईआरटी द्वारा कक्षा ग्यारह की इतिहास की 2001 में पुनर्मुद्रित पुस्तक पढ़ें। लेखक गुरु के बलिदान और उसके पीछे की दृढ़ता को बिल्कुल भी वर्णित नहीं करता है। वह तो औरंगजेब की क्रूरता और मतांधता पर पर्दा डालने से भी नहीं हिचकता है। गुरु तेग बहादुर साहिब के मासूम बच्चों के साथ जो क्रूरता की गई और उन बच्चों ने मतांतरण न करने में जो साहस दिखाया उस पर भी लीपापोती का पूरा प्रयास किया गया। मई 2004 के बाद यही पुरानी पुस्तकें वापस लाई गईं। नई सारी की सारी हटा दी गईं। यह कैसी विडंबना है कि स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने के बाद ही गुरु तेग बहादुर साहिब का और उनके सुपूतों को ठीक ढंग से पहचाना गया और वीर बाल दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ की गई है। खिलवाड़ केवल सिख गुरुओं के योगदान से ही नहीं किया गया, बल्कि जैन और जाट समाज के संबंध में भी इतिहास को कुछ यों तोड़ा-मरोड़ा गया जो सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किए गए उस शपथपत्र की याद दिलाता है जिसमें राम के अस्तित्व को पूरी तरह नकार दिया गया था। इसे जब वर्ष 2001 में हटाया गया तो वह भगवाकरण कहा गया, लेकिन जो लोग इसे मई 2004 में वापस लाए, उन्होंने दो-तीन वर्ष बाद हरियाणा के विधानसभा चुनावों में जाट समुदाय के घोर विरोध के कारण इसे फिर से हटा दिया! आम लोगों के लिए यह सब समझ पाना सरल नहीं है, लेकिन इतना तो सभी जान सकते हैं कि यह इतिहास वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं था। एनसीईआरटी को लगातार विद्वानों, नागरिकों तथा संस्थाओं से तथ्यात्मक सुधार करने के अनुरोध और प्रतिवेदन मिलते रहे, लेकिन जाने-माने वामपंथी-मार्क्सवादी तत्वों ने कोई सुधार होने ही नहीं दिया। अब इतिहास में सुधार हो रहा है तो यही लोग एक बार फिर शोर मचा रहे हैं।
 Date:10-07-23
Date:10-07-23
चीन की नई चुनौती
संपादकीय
चीन ने गैलियम से बनने वाले आठ उत्पादों और जर्मेनियम से बनने वाले छह उत्पादों के निर्यात पर नियंत्रण लगाने का निर्णय लिया है जिससे सेमीकंडक्टर उद्योग में आपूर्ति क्षेत्र की अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। यह उन सभी उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों को प्रभावित करेगा जिनमें चिप का इस्तेमाल होता है। यह सीधे तौर पर अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ का प्रतिकार है जिन्होंने उच्च सेमीकंडक्टर उपकरणों का चीन को निर्यात रोक रखा है। भारत की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन पहल मसलन 76,000 करोड़ रुपये मूल्य का ‘सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम’ भी बाधित हो सकता है। आपूर्ति की बाधाएं कई उद्योगों में उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। चीन से निर्यात को लाइसेंस की आवश्यकता होगी और यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रक्रिया कितनी दुष्कर होगी। वर्ष 2022 में चीन ने दुनिया का 98 प्रतिशत गैलियम और 67 फीसदी से अधिक जर्मेनियम उत्पादित किया। बॉक्साइट अयस्क की खदानों के मिलने के बाद भारत में एल्युमीनियम का उत्पादन शुरू हुआ और उसके सह उत्पाद के रूप में मामूली मात्रा में गैलियम निकलना शुरू हुआ। बहरहाल जर्मेनियम के मामले में हम पूरी तरह आयात पर निर्भर है। हालांकि कुछ श्रेणी के कोयले तथा जस्ते के अयस्क में यह कुछ मात्रा में पाया जाता है। दोनों धातुएं भारत के महत्त्वपूर्ण खनिज की सूची में शामिल हैं।
गैलियम का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर के सर्किट बोर्ड, एलईडी उपकरणों, थर्मामीटर और बायोमेट्रिक सेंसर आदि में होता है। जर्मेनियम का इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर, सोलर सेल, कैमरा और माइक्रोस्कोप लेंस तथा इन्फ्रारेड नाइट विजन सिस्टम में होता है। हर कारोबार और शोध एवं विकास प्रयोगशाला जिसे इन दोनों धातुओं की आवश्यकता होती है, वह चीन के निर्यात लाइसेंस के लिए जूझ रही है। आपूर्ति बाधित होने की आशंका से कीमतों में उछाल आई है। ऐसे में दुनिया भर में विकल्पों की तलाश तेज होगी। व्यापक तौर पर देखें तो ऐसे अन्य अहम प्राकृतिक संसाधनों की तलाश जोर पकड़ सकती है जिनकी आपूर्ति में चीन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। फिलहाल सरकार ने उद्योग जगत को आश्वस्त किया है कि भारत को गैलियम और जर्मेनियम की कमी का सामना नहीं करना होगा। बहरहाल, अहम और उभरती तकनीक यानी आईसेट पर भारत-अमेरिका की पहल जहां भविष्य में ऐसी धातुओं की आपूर्ति में मददगार हो सकती है, वहीं अस्थायी तौर पर आपूर्ति बाधित रह सकती है।
गैलियम और जर्मेनियम दुर्लभ नहीं हैं लेकिन चीन इकलौता ऐसा देश है जिसने इन दोनों धातुओं के खनन और परिशोधन में निवेश किया है इसलिए वही इसका किफायती उत्पादक है। जिन अन्य देशों के पास इसका भंडार है उन्हें परिशोधन सुविधा स्थापित करनी होगी। लेकिन इसमें वर्षों का समय लग सकता है और यह प्रश्न बरकरार है कि क्या वैकल्पिक आपूर्ति लागत में चीन का मुकाबला कर पाएगी या नहीं। चीन कई अन्य दुर्लभ धातुओं तथा लीथियम का अहम आपूर्तिकर्ता है। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण तथा सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इन दुर्लभ धातुओं की आवश्यकता होती है। बिजली चालित वाहनों की तकनीक लिथियम-आयन बैटरी के इर्दगिर्द है। गैलियम और जर्मेनियम का निर्यात अचानक सीमित करने से अन्य देश वैकल्पिक आपूर्ति तैयार करने पर विचार कर सकते हैं।
जीवाश्म ईंधन की भूराजनीति जहां जटिल है। वहां पेट्रोलियम निर्यातक देशों के समूह ओपेक में 23 सदस्य हैं जबकि गैर ओपेक देशों में अमेरिका और कनाडा शामिल हैं। ऐसे में जीवाश्म ईंधन के आयातकों को किसी विपरीत परिस्थिति में विकल्प मिल सकते हैं। दुर्लभ संसाधनों, लीथियम, गैलियम, जर्मेनियम और ऐसी अन्य धातुओं की भूराजनीति और अधिक जटिल हो सकती है क्योंकि इनका केवल एक ही बड़ा निर्यातक है। हरित ईंधन की ओर बदलाव और उच्च तकनीक आधारित उद्योग विकसित करने की कोशिशों को तब धक्का पहुंच सकता है जबकि चीन अन्य खनिजों पर भी ऐसे निर्यात प्रतिबंध लगा सकता है। चीन के एकाधिकार और भारत-चीन के कठिनाई भरे रिश्तों को देखते हुए भारत को हालात से बहुत सावधानी से निपटना होगा।
Date:10-07-23
विचारधारा का अंत और उसका पुनर्जन्म
शेखर गुप्ता
पिछले दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में जो नाटकीय परिवर्तन नजर आया वह हमारी राष्ट्रीय राजनीति के बारे में दिलचस्प झलक पेश करता है। वह बताता है कि फिलहाल हम कहां हैं, हम यहां तक कैसे पहुंचे और हमारा अगला पड़ाव क्या है?
इसके बाद कुछ अन्य दिलचस्प सवाल आते हैं। क्या राजनीति में अभी भी विचारधारा मायने रखती है? अगर आम आदमी पार्टी के उदय पर नजर डालें तो आपको लग सकता है कि नहीं रखती।
भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और मुफ्त में चीजें देने के वादों से विचारधारा नहीं बनती। भले ही दीवार पर आंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें ही क्यों न लगी हों।
दूसरी ओर यही निष्कर्ष महाराष्ट्र के घटनाक्रम के आधार पर भी निकाला जा सकता है: पहले शिव सेना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अलग होकर विचारधारा के लिहाज से अपने प्रतिद्वंद्वियों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस से मिली। बाद में शिव सेना के विधायकों का बड़ा हिस्सा दोबारा भाजपा से मिल गया। यहां विचारधारा और सिद्धांतों की बात करना बेमानी है। राकांपा नेता और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल ने पत्रकारों से बात करते हुए अपने भाजपा नीत गठबंधन में जाने और मौजूदा राजनीति के बारे में जानकारी प्रदान की।
जब उनसे इस विचारधारात्मक बदलाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर राकांपा को शिवसेना के साथ जाने में दिक्कत नहीं थी तो अब भाजपा के साथ जाने में क्या समस्या है?
मुझे कहीं शरद पवार की भी टिप्पणी देखने को मिली जिसमें उन्होंने कहा कि शिव सेना के समावेशी हिंदुत्व में समस्या नहीं है लेकिन भाजपा के हिंदुत्व में है।
तथ्य यह है कि अगर खुले दिमाग से व्यापक तस्वीर पर नजर डाली जाए तो विचारधारा अब कुछ दशक पहले की तुलना में अधिक मजबूत शक्ति बनी है लेकिन यह केवल एक पक्ष में नजर आती है और वह है भाजपा।
दूसरी ओर, कई नेता और उनके दल इन दशकों में बिना किसी विचारधारात्मक माहौल के पनपे हैं और उनके सिद्धांत और उनकी प्रतिबद्धताएं सत्ता के साथ रही हैं।
महाराष्ट्र की राजनीति में बीते चार साल में जो कुछ हुआ वह हमें बताता है कि शायद यह दौर भी अब समाप्त हो रहा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राकांपा को सत्ता में अपनी छोटी पारी का सुख भोगने को मिलेगा लेकिन चुनावी और राजनीतिक दृष्टि से उनकी राजनीतिक शक्ति का पराभव ही होगा।
इस तरह लेनदेन की राजनीति करने वाले दो प्रमुख दलों के अंत की शुरुआत हो सकती है। बीते 25 सालों के दौरान दिल्ली की सत्ता पर काबिज गठबंधन में इनमें से कोई न कोई दल हमेशा शामिल रहा है।
मोदी के पहले के समय में खासतौर पर 2009 के चुनाव के बाद हममें से कई लोगों ने विचारधारा रहित भारतीय राजनीति का स्वागत किया था। हमने निष्कर्ष निकाला था कि अत्यधिक युवा मतदाता वोटिंग मशीन का बटन दबाते समय केवल एक बात का ध्यान रखते हैं: इसमें मेरा क्या फायदा है? नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव अभियान में इस बात का ध्यान रखा था लेकिन उनकी व्यापक अपील हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद की थी।
वह बार-बार पाकिस्तान का जिक्र करते थे और परोक्ष रूप से मुस्लिमों का भी। खासतौर पर ‘गुलाबी क्रांति’ (मांस निर्यात का चुनावी कोड) का जिक्र करते हुए। दूसरी ओर कांग्रेसनीत विपक्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तथा अन्य अधिकार आधारित कानूनों और कल्याण योजनाओं के सहारे था।
2019 तक मोदी ने और कठोर हिंदुत्व को अपना लिया यानी पुलवामा/बालाकोट के बाद। जबकि इस बीच कांग्रेस राफेल, चौकीदार चोर है आदि के जरिये भ्रष्टाचार के आरोपों के सहारे मैदान में थी। उसने न्याय योजना के सहारे नई तरह की कल्याण योजना पेश करने का प्रयास किया। स्पष्ट वैचारिक विभाजन तब तक तैयार नहीं हुआ था। अगर कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ा तो भाजपा से लड़ रहे छोटे दलों के हश्र का अंदाजा लगाया जा सकता है।
अलग दिखने की उनकी कोशिश या तो मुस्लिमों के संरक्षण पर आधारित थी या फिर मतदाताओं को नि:शुल्क सुविधाएं देने के बारे में। कुछ क्षेत्रीय दलों मसलन द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम और केरल में वाम दलों को छोड़ दिया जाए तो भाजपा के अलावा किसी दल ने विचारधारा के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा। इससे मोदी के लिए लड़ाई आसान हो गई।
यह बात सन 1984 के बाद की राजनीति में प्रमुख है और इसलिए हम इसका बार-बार जिक्र करते हैं। हम सन 1984 को इसलिए बीच में रख रहे हैं कि उस वर्ष राजीव गांधी 415 लोक सभा सीटों के साथ सत्ता में आए थे। उसके बाद भारत पर कौन शासन करेगा इसका निर्धारण इस बात से होता आया है कि धर्म के आधार पर बनी एकजुटता को कोई जाति के आधार पर कोई कितना तोड़ सकता है? या फिर जाति में बंटे लोगों को कोई कितना एकजुट कर सकता है? इस अवधि में शुरुआती 25 वर्ष जातीय ताकतें जीतीं जबकि उसके बाद मोदी युग आ गया।
इन्हीं 25 वर्षों में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति भ्रमित हो गई और अपनी वैचारिक धार गंवा बैठी। भाजपा का विरोध बड़े सिद्धांत के रूप में सामने आने के बजाय मुस्लिम वोट पाने का जरिया भर नजर आने लगा।
इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष मत मुस्लिम मतों का पर्यायवाची बन गया। इसके बाद विभिन्न दलों के बीच टकराव आरंभ हुआ। मसलन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, वाम दल और तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस तथा नई मुस्लिम ताकतों मसलन असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम तथा असम में बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ में भी ऐसा ही देखने को मिला। महाराष्ट्र के अलावा अधिकांश राज्यों में राकांपा ने अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए। 2017 के गुजरात चुनावों में भी उसने अपने प्रत्याशी उतारे।
इस बीच भाजपा अपनी हिंदू राष्ट्रवादी छवि को निरंतर और तीक्ष्ण बनाती जा रही है। ‘सबका साथ, सबका विकास’ का उसका नारा भी उस नए आत्मविश्वास को दिखाता था कि उसे पता है मुस्लिम उसे वोट नहीं देते लेकिन उनका उत्पीड़न नहीं होगा। इससे राष्ट्रीय राजनीति एकतरफा होती गई। हालांकि कई राज्यों में भाजपा क्षेत्रीय दलों को हराने में नाकाम रही।
केरल और तमिलनाडु को छोड़कर अधिकांश राज्यों में उसे एक नेता या परिवार वाले दलों से चुनौती मिली। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र शामिल हैं। इन दलों में से अनेक को पुनर्विचार करने की जरूरत है। परिवार टूट सकते हैं, भतीजे अपने चाचाओं को छोड़ सकते हैं, वफादारों को लुभाया जा सकता है या एजेंसियों से उन पर दबाव बनवाया जा सकता है। प्रफुल्ल पटेल की तरह उन सभी के पास कोई न कोई दलील होती है।
बीते दिनों नई दिल्ली के नेहरू स्मृति पुस्तकालय में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर भाषण देते हुए लेखक-संपादक टी एन नाइनन ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि अगर शास्त्री की असमय मृत्यु नहीं हुई होती तो एक संभावना यह थी कि शायद कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ होता या शायद इंदिरा गांधी की जगह वाई बी चव्हाण उत्तराधिकारी बनते।
उन्होंने कहा कि अगर 1969 में इंदिरा गांधी ने पार्टी का विभाजन नहीं किया होता तो शायद पार्टी शायद इतनी तेजी से वाम रुझान नहीं लेती जैसा कि उसने उनके नेतृत्व में लिया। उन्होंने अपने ही दल के पुराने नेताओं से निपटने के लिए ऐसा किया। मेरी दृष्टि में यह विचारधारा आधारित बदलाव नहीं बल्कि सुविधा की लड़ाई थी। रूढि़वादी बुजुर्गों से निपटने के लिए प्रगतिशील, युवा वाम से बेहतर भला क्या होता?
परंतु इस प्रक्रिया में कांग्रेस के पास ऐसी विचारधारा बची जिस पर उसके कार्यकर्ता खासकर शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह यकीन नहीं करता था। शायद यही वजह है कि तब से औसतन हर पांच साल में पार्टी का विभाजन होता रहा। अलगाव के बाद ज्यादातर धड़े क्षेत्रीय ताकत बन गए। राकांपा से लेकर मेघालय में संगमा, तृणमूल कांग्रेस और वाईएसआरसीपी इसमें शामिल हैं। दूसरी ओर भाजपा ने अपना वैचारिक और राजनीतिक सामंजस्य बनाए रखा। बीएस येदियुरप्पा और कल्याण सिंह जैसे कुछ नेता पार्टी से बाहर भी गए तो लौट आए। शंकर सिंह वाघेला जैसे नेता जो कभी नहीं लौटे वे धीरे-धीरे परिदृश्य से गायब हो गए।
इससे मौजूदा राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति पता चलती है। महाराष्ट्र से भी यही संदेश निकल रहा है। अगर कांग्रेस अपनी ताकत बटोरकर एक आधुनिक विचारधारा को अपना सके तो हम दो दलीय परिदृश्य की ओर जा सकते हैं।
अपनी समस्याओं का इलाज नहीं खोज पा रहा यूरोप
हर्ष वी पंत, ( प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन )
पिछले कुछ दिनों से फ्रांस को झुलसा रही आग दरअसल वर्षों से सुलग रही थी। कुछ-कुछ वर्षों के अंतराल पर हमने फ्रांस की सड़कों पर ऐसे ही दृश्य देखे हैं, जिनमें परस्पर संघर्ष में जुटे विभिन्न पक्ष एक ही तरह के तर्क दोहराते रहे हैं, पर तात्कालिक रूप से संकट टलने के बाद बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने की कोशिश नदारद रही है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जिनको अच्छी तरह से समझा जाता है, लेकिन उनका समाधान नहीं किया जाता है। फ्रांसीसी राज्य और समाज के लिए चुनौतियां गंभीर हैं, पर यहां का राजनीतिक नेतृत्व कठिन विकल्पों से बचता रहा है।
इस बार उपद्रव तब शुरू हुआ, जब पिछले हफ्ते एक फ्रांसीसी पुलिस अधिकारी ने पेरिस के उपनगर नान्टेरे में यातायात रोकने के दौरान अल्जीरियाई और मोरक्कन मूल के 17 वर्षीय किशोर नाहेल मेरजौक की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके विरोध में घातक दंगे हुए, पेरिस के कई उपनगर हिंसा की चपेट में आ गए। हिंसा शहर के केंद्रों तक पहुंच गई, जहां भीड़ ने अनेक इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। लुटेरों और आगजनी करने वालों ने इसका उपयोग और अधिक असंतोष पैदा करने के लिए किया। यह सबसे गंभीर सामाजिक गड़बड़ी है, जिसे फ्रांस 2005 से देखता आ रहा है। तब दो किशोरों की आकस्मिक मौत ने जातीय अल्पसंख्यकों को सड़कों पर उतार दिया था।
फ्रांस में पुलिसिया व्यवस्था काफी समय से सवालों के घेरे में रही है। हालिया हत्या कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि इस साल ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोकने के दौरान हुई हत्या की यह तीसरी घटना थी। पिछले साल ऐसी 13 हत्याएं हुई थीं। ज्यादातर पीड़ित अश्वेत या अरब मूल के थे, जिससे यह धारणा मजबूत हुई कि फ्रांसीसी पुलिस पुख्ता तौर पर नस्लवादी है। इस पहलू को संयुक्त राष्ट्र भी पहले उजागर कर चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के लिए यह गंभीर संकट है। उनका प्रशासन पिछले कुछ महीनों से विरोध-प्रदर्शनों से परेशान है। राष्ट्रपति अपने देश की वैश्विक स्थिति को ऊपर उठाने में लगे हैं, पर घरेलू समस्याएं मुश्किलें पैदा कर रही हैं। इस बीच, पेरिस अगले साल ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला है। समस्या यह भी है कि मैक्रॉन को वामपंथी और दक्षिणपंथी, दोनों परेशान कर रहे हैं। वैसे, 2005 के विपरीत इस बार आपातकाल की घोषणा नहीं हुई, पर 40,000 से ज्यादा पुलिस अफसरों की तैनाती के बावजूद दंगा नियंत्रण में समय लग गया।
फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जातीय अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के मामले भी उभर आए हैं। फ्रांस की राजनीति बंटी हुई है। सामाजिक-आर्थिक विभाजन व इसके नतीजों से निपटने की दिशा में कोई संस्थागत बदलाव कहीं भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में, ताजा संकट फ्रांस में समुदायों के बीच विभाजन बढ़ाएगा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रतिक्रिया की भी प्रबल आशंका होगी। दरअसल, पूरे यूरोप में आप्रवासियों के खिलाफ भावनाएं नकारात्मक हो रही हैं और इससे धुर दक्षिणपंथी पार्टियों को फायदा हो रहा है। फ्रांस में हालिया दंगों का इस्तेमाल धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन ने मैक्रॉन को निशाना बनाने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि कायरता व समझौतों की फ्रांसीसी भयानक कीमत चुका रहे हैं ।
ऑस्ट्रिया से इटली, ग्रीस से स्वीडन तक, सुदूर दक्षिणपंथी पार्टियां यूरोप में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि पहचान के मुद्दे जटिल हो गए हैं और उन्हें पारंपरिक मूल्यों पर हमला होता दिख रहा है। मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के पास उचित जवाब नहीं है और वे ऐसी भाषा बोल रहे हैं, जिससे अधिकांश लोग जुड़ नहीं पाते। ऐसे में, आम लोगों को दक्षिणपंथ की स्पष्टता आकर्षक लग सकती है। जब आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही हैं, तब नेतृत्व की कमी से भी दक्षिणपंथी राजनीतिक संस्थाओं को फायदा हुआ है। लोगों की अभिव्यक्ति में आप्रवासी विरोधी भावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। स्वीडन में धर्मग्रंथ जलाने की हालिया घटना, ब्रिटेन में आप्रवासन से निपटने के लिए नए कानून और फ्रांस की सड़कों पर दंगे, ये सब यूरोप की व्यापक बीमारी के लक्षण हैं, जिनके गंभीर दीर्घकालिक परिणामों की आशंका पुरजोर है।
