
09-09-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:09-09-20
Date:09-09-20
No Questions, Mr Speaker
To use the pandemic as an excuse to restrict Parliament is highly disingenuous
Sagarika Ghose, [ Sagarika Ghose has been a journalist for over three decades, starting her career with The Times of India ]
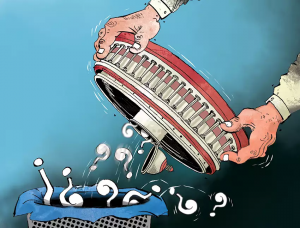
Vajpayee followed the example of his self-confessed role model, Jawaharlal Nehru, the original parliamentarian-PM who not only attended Parliament almost every day but prepared painstaking replies to all questions directed at him. Nehru and Vajpayee would have recoiled in horror at the Modi government’s recent decision to virtually abandon a long established parliamentary tradition – question hour.
Question hour in Parliament is an hour when MPs get to cross-question and interrogate ministers on urgent issues, a crucial democratic institution by which peoples’ representatives hold a powerful executive accountable. The government last week decided that for the upcoming monsoon session it was going to “do away temporarily with question hour due to the extraordinary situation caused by Covid”. Question hour is to be drastically truncated: No questions can be asked extempore, only written questions are to be submitted beforehand to which ministers will give scripted answers.
To use Covid as an excuse to restrict Parliament is highly disingenuous. In fact, it is now more crucial than ever that the government is questioned on access to healthcare and mass unemployment. However, in India coronavirus is seriously endangering the health of democracy by increasing the stranglehold of government and disenfranchising citizens. The pandemic is leading to a dangerous spike in state power and a loss of basic citizens’ rights and freedoms, a democracy deficit which may haunt us even after Covid recedes.
Yet even before Covid, there’s been a systematic dilution of parliamentary practices with ceaseless disruptions and decreasing time for genuine debate and questions. Neither Modi, nor the principal face of the opposition Rahul Gandhi, have distinguished themselves in Parliament. Rahul opted not to lead his party in the House, choosing Mallikarjun Kharge in 2014 and Adhir Ranjan Chowdhury in 2019, the latter known primarily for feisty lung power than parliamentary intellect.
In the 16th Lok Sabha, Rahul didn’t ask a single question in question hour. Modi hardly devotes much time to the cut and thrust of parliamentary debate, staying silent during contentious parliamentary debates like triple talaq and Article 370 last year.
The main reason for the rising disdain for Parliament among top politicians is the increasing disjunction between electability and parliamentary performance. You don’t need Parliament to win elections. In previous decades, fiery parliamentary talents like Bhupesh Gupta, Nath Pai, Minoo Masani or Vajpayee derived their political standing from their parliamentary record. Today a media-saturated politics has created personality cults which short-circuit Parliament. National and state elections are fought around the personality of the supreme leader, so that most individual MPs and MLAs are faceless, lacking their own identities. They are surrogates coasting along in the backwash of a supremo-centred wave. It was the Modi persona that dominated a majority of the 543 Lok Sabha constituencies in 2014 and 2019. At the start of Covid, MPLADS (financial allotments to MPs for development work) was suspended, further reducing MPs’ status and links with their constituencies. In Bengal Mamata Banerjee is a similarly dominant leader. In fact question hour has also been cancelled in the forthcoming Bengal assembly session.
Parliament is also becoming irrelevant because of the fundamental de-legitimisation of debate across our intensely polarised society. Because of this deep divide across all levels of society asking any kind of question is seen as politically motivated or loaded with “agenda”. Only when genuine debate – and not the meaningless TV shouting match – is re-legitimised, can Parliament see the return of substantive debate.
A polarised society is bound to have a dysfunctional Parliament. An example of political hyper polarisation was seen in the recent controversy over the parliamentary standing committee on IT and its decision to summon Facebook for allegations of political bias. Parliamentary committees are supposed to be bipartisan spaces to take up citizens’ issues. Instead there was an unseemly confrontation between BJP’s Nishikant Dubey and the chairman Congress’s Shashi Tharoor for summoning Facebook in the first place. Instead of Facebook being asked to explain itself, politicians publicly scrapped with each other.
Governments with hefty majorities scorn parliamentary norms. There is the normalisation of the ordinance route. Ordinances were meant for extraordinary situations but today they’re freely used signalling an impatience with debate. From the nullification of Article 370 which was rammed through without an extended debate to amendments to the Aadhaar Bill which in 2016 was passed as a money bill (requiring only a yes in the Lok Sabha), government diktats have taken the place of legislative deliberations. Importantly, there’s also been a steady decline in the number of days Parliament sits. The first Lok Sabha had 677 sittings, the 16th only 226. When a government refuses to be questioned or challenged, Parliament ceases to matter.
In fact in India the more powerful a politician, the less likely they are to submit to no-holds-barred questioning, seen in the fact that neither Sonia Gandhi nor Modi hold open press conferences. This regal scorn for questions befits a monarchy, not a modern 21st century democracy.
Ironically, while downsizing the value of parliamentary traditions, the Modi government has proposed constructing a new Parliament building under its new Central Vista project. But instead of another brick and mortar structure, gleaming on the outside but potentially hollow on the inside, why not build better democracy within Parliament instead?
FARMERS UP THE GARDEN PATH
They are paying more, even under schemes meant for their benefit
Ajay Vir Jakhar, [ The writer is chairman, Bharat Krishak Samaj ]

Under PM Kisan, each landowning farmer (landless are excluded) receives Rs 6,000 annually. As per a Punjab Agriculture University study, a farmer growing a combination of paddy and wheat utilises about 50 litres of diesel per acre. The diesel usage differs, depending on the crop and practices. Today, each litre of diesel gets taxed at about Rs 45. Even if one is to discount the average country-wide diesel usage per acre to 60 per cent — 30 litres — the government is virtually collecting a tax of Rs 1,200 per acre from farmers. A small five-acre farmer could be paying about Rs 6,000 as diesel tax, the same as the largesse being received. Additionally, the single-tax regime, which parliamentarians had celebrated at the midnight hour, has farmers paying GST on purchase of inputs like seeds, pesticides, fertilisers, tractors and implements and such others for which, unlike industry, they cannot claim input credit.
Second, when international crude price was at $60 per barrel in July 2019, the Ujwala-scheme-subsidised gas cylinder was available to the underprivileged in my village at Rs 503. Then came COVID-19, the establishment floundered, government revenues evaporated, the economy tanked and crude prices fell to stabilise at about two-thirds the price at $40. When everything was reeling downwards, by this July, the price of the subsidised cylinder increased by nearly a fourth to Rs 611. Incredibly, the government is collecting more per cylinder from the poorest sections of society when it is popularly perceived to be providing increased financial support to them. Broadly, each of these poverty alleviation programmes seems to have a recurring theme — being funded by the poor themselves.
Third, earlier this year, amid the COVID clampdown, the MSP for paddy was increased by 2.9 per cent, while even the CACP report on which this MSP is based, projected an increase of 5.1 per cent in the composite input price index for 2020-21 over 2019-20, indicating a higher cost of cultivation. Even the food inflation in cereals for 2019 was 8.4 per cent. In real terms, the MSP for paddy will decrease by the time of marketing in October. In 2018, in the run-up to the 2019 parliamentary elections, the government magnanimously raised MSP for paddy by 12.9 per cent. Having attained a resounding victory, thereafter the increases in MSP have been minuscule at 3.7 per cent in 2019 and 2.9 per cent in 2020. The BJP’s allies like the Akali Dal in Punjab and Lok Dal offshoots in Haryana, who had attained power on farmers’ votes, have become self-serving, subservient caricatures of their glorious past. The pain of the betrayal is excruciating.
The MSP has changed from being the minimum support price to becoming the maximum selling price. It is not surprising that the demand for MSP as a legal right has begun to resonate in the field.
Lastly, without digging too deep, one can find policies continuing during COVID times emanating in ministries other than agriculture which impact the food value chain and are counterproductive and conflicting. For example, 75 per cent of the dal consumed in India is chana and arhar. While both are selling below MSP, import duties on masoor dal were reduced by two-thirds to 10 per cent because there was a demand for it in one part of India. My core contention is more fundamental: If a consumer can afford to eat a more expensive dal or a more expensive non-essential produce (say, onions), then they don’t need to be subsidised by subduing farmgate prices. A reset in approach to mitigating inflation is a must.
Even though different wings of the government are seemingly working at cross purposes, issues of governance aren’t fatally flawed, but perfectible. The government, however, chooses to hide behind hollow euphemisms that conceal the truth of its realpolitik strategy to suppress farmgate prices to keep the urban consumer from becoming restless and find a common cause for protest. It is the same worry that gnaws at authoritarian regimes across the world. The journey to “achhe din” has until now led farmers up on an anfractuous path to nowhere in particular. When the PM, a man of unyielding perseverance, connects the dots in the future looking backwards, he will find a fractured legacy of unresolved challenges he thought he had solved.
A case for down-to-earth governance
Strong local governance remains the unfinished agenda to make India’s democracy strong and deep
Arun Maira is Former Member, Planning Commission and author of ‘Redesigning the Aeroplane While Flying: Reforming Institutions’
Nine years ago, Anna Hazare ended his historic fast when the Prime Minister, Manmohan Singh, informed him that Parliament had expressed support for proposed changes to anti-corruption legislation; “the ‘sense of the House’ was behind Anna Hazare’s key demands”. The historic bending of Parliament to the people’s will was the result of a remarkable movement of citizens — rich, middle class, and poor — coming together to take politics back from politicians and to demand Parliament’s accountability to citizens. Since then the nation’s attention has moved on, from weaknesses in institutions of governance, to threats from China on the nation’s borders and to global problems caused by COVID-19.
Hazare’s point
The single point demand of the Anna movement was the institution of the Jan Lokpal to try all government functionaries when accused of corruption; even the Prime Minister. Anna Hazare is a controversial person. However, one should not throw the baby out with the bathwater, and the thought he left while breaking his fast is worth recalling. He said Lokpals and Lokayuktas would not eliminate the root causes of corruption in politics and government. Electoral reforms and decentralisation of power were essential.
Parliamentarians of all parties were affronted by the claims of leaders of the Anna movement that they were the representatives of the people rather than the Parliamentarians. They taunted leaders like Arvind Kejriwal to prove it by winning elections. This spurred the formation of the Aam Aadmi Party. It joined the system which had to be reformed and had to play the game by the system’s rules. This dismayed many and the movement for fundamental reforms of governance lost its steam.
It is about money
Around the world, electoral democracies have become infected by the disease of funding political parties and elections. Money is required to win elections legitimately, even when people are not bribed to vote, which is illegitimate. Communications with citizens, essential for democracy, can be very expensive. Advertisements have to be paid for as well as teams of professionals for managing social media. If one party raises a million to spend, and the other raises two million, the first must raise even more or its million would have been wasted were it to lose the election. Thus, the race to raise more money for legitimate electioneering purposes can corrupt the process of funding parties and elections. Solutions are not easy because the right to free speech, and to put one’s money where one’s mouth is, is a fundamental right that cannot be denied as the Supreme Court of the United States ruled.
The debate continues about which is a better system. A presidential system, like the U.S. or the French one; or a parliamentary system, like the British one which India has adopted. Though the U.S. has a presidential system it cannot implement reforms to its flawed health-care system nor control the spread of dangerous weapons because party divisions within its democratically-elected Congress and Senate seem to make it impossible. Debates within India’s Parliament, in which all members have been elected by the world’s most impressive election machinery, hardly inspire citizens’ confidence in their representatives’ ability to govern the country.
Process and deliberations
The problem in electoral democracies is not only with the process by which representatives are elected, but also in the conduct of their deliberations when they come together. This problem is not due to the quality of the individuals — whether they are ‘educated’ or not or even whether they have criminal records or not. It is inherent in the design of the process for electing representatives.
The framers of the U.S. Constitution had worried about this problem. Representatives of the people must be chosen by smaller electorates within geographical constituencies. However, when they meet together in the national chamber, they are expected to govern the whole country. They must shed their local hats and put on a national hat to consider what will be best for the whole country. However, if the people who elected them find they are not protecting local interests, they will not be elected again. Constituency favouring leads to challenges for equitable solutions for sharing of river waters, and to railway stations where there are very few people, because representatives fight for the largest share of the pie for their constituency rather than the growth of the whole pie.
Electing good representatives to Assemblies is not enough to ensure good decisions will be made. Imagine 500 representatives in a chamber, each clamouring for his constituencies’ interests. How will decisions be taken? As James Madison wrote in The Federalist paper No.55 (https://bit.ly/3h7Pn9V), “had every Athenian citizen been a Socrates, every Athenian assembly would still have been a mob.”
Inner democracy
Political parties in electoral democracies provide a solution to the problem of creating an alignment of views among representatives from hundreds of constituencies around the country. A party’s point of view on fundamental matters can unite many. Therefore, all representatives need not be heard from in Parliament. One can speak for many. It is easier to form effective governments in electoral democracies when there are fewer parties. When there are too many parties and too many contradictory points of view to be accommodated within a coalition, governance can break down. Therefore, political parties are not evil. However, when political parties are not internally democratic, they become reviled as the means for self-aggrandising politicians to amass power and wealth, and democratic nations suffer.
It has become very difficult in representative democracies, for reasons explained here, to arrive at good and fair decisions for the governance of a large state or country. It is tempting to abandon political parties and parliaments and revert to direct forms of democracy where every decision can be put directly to all citizens to vote on. New Internet technologies make this possible. But, if all voters have not understood what is at stake, they cannot decide well, as Californians have learned over decades with their forms of direct democracy, and the U.K. has too with its hasty Brexit referendum.
Complex issues, where many interests collide, must be resolved by reason, not settled by the numbers. Hence there is no alternative to good local governance, wherein citizens manage their local affairs democratically. Locals know best how to balance the preservation of their water sources while making it easier for local enterprises to do business, and how to make their local schools and health facilities accessible to all citizens. One-size solutions devised by experts at the centre cannot fit all: therefore, local systems solutions are essential to solve global systemic problems of environmental sustainability and inclusive growth.
Citizens must solve issues
No doubt, electoral funding must be cleaned up, and democracy within political parties improved to make representative democracy work better. This will require big changes to entrenched systems, yet will not be sufficient for good, democratic governance. Citizens must appreciate that they have to be the source of solutions, and not become only the source of problems for governments and experts to solve for them.
Citizens must learn to listen to each other’s perspectives in their villages and in their urban neighbourhoods. Those with the most needs in the community must be enabled to participate, alongside the most endowed, in finding solutions for all. Since India’s Independence 73 years ago when the power of government was transferred from a centre in London to a centre in Delhi, strong local governance remains the unfinished agenda to make India’s democracy strong and deep.
Date:09-09-20
What is in a NAM and India’s alignment
The country has not yet found a universally accepted successor, as a signature tune for its foreign policy
P.S. Raghavan, a former diplomat, is Chairman of the National Security Advisory Board.
India’s External Affairs Minister, S. Jaishankar, said recently that non-alignment was a concept of relevance in a specific era and a particular context, though the independence of action enshrined in it remains a factor of continuity in India’s foreign policy. This is about as explicit an assertion as one is likely to get from our political leadership of an obvious post-Cold War fact: that non-alignment, as a foreign policy concept, is dead.
United by a campaign
Non-alignment was a policy fashioned during the Cold War, to retain an autonomy of policy (not equidistance) between two politico-military blocs. The Non-Aligned Movement (NAM) provided a platform for newly independent developing nations to join together to protect this autonomy. It was a disparate group from many continents, with varying degrees of proximity to, and dependence on, one or the other bloc; and broadly united around NAM’s flagship campaigns for de-colonisation, universal nuclear disarmament and against apartheid.
One of the blocs was disbanded at the end of the Cold War. De-colonisation was largely complete by then, the apartheid regime in South Africa was being dismantled and the campaign for universal nuclear disarmament was going nowhere. Freed from the shackles of the Cold War, the NAM countries were able to diversify their network of relationships across the erstwhile east-west divide. Non-alignment lost its relevance, and NAM its original raison d’être.
For a few years now, non-alignment has not been projected by our policymakers as a tenet of India’s foreign policy. However, we have not yet found a universally accepted successor as a signature tune for our foreign policy. Successive formulations have been coined and rejected. Strategic autonomy was one, which soon acquired a connotation similar to non-alignment, with an anti-U.S. tint. Multi-alignment has not found universal favour, since (as the External Affairs Minister said elsewhere) it may convey the impression of opportunism, whereas we seek strategic convergences. Seeking issue-based partnerships or coalitions is a description that has not stuck. “Advancing prosperity and influence” was a description Dr. Jaishankar settled for, to describe the aspirations that our network of international partnerships seeks to further.
China factor
In the wake of the current stand-off with China, there have been calls for India’s foreign policy to shed its inhibitions and make a decisive shift towards the United States, as the only viable option to counter China. The government has been more nuanced in its approach. The External Affairs Minister clarified that a rejection of non-alignment does not mean a rush to alignment: India will not join an alliance system.
The fact is that ‘alliance’ is as much a Cold War concept as non-alignment. During the Cold War, the glue that held countries of an alliance together was composed (in varying proportions) of ideological convergence and an existential military threat. With the disintegration of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) and the Warsaw Pact, this glue dissolved and the international options of alliance partners widened, just like those of NAM countries. The strategic interests of alliance partners are no longer congruent. This is evident in the Euro-Atlantic alliance. U.S. President Donald Trump’s words and deeds have highlighted divergences within the North Atlantic Treaty Organization (NATO), and even widened them, but strains have periodically surfaced even earlier — over the 2003 U.S. invasion of Iraq, for example, or on policy towards Russia or West Asia. Turkey is constantly exploring the limits of NATO discipline.
Alliances in the Asia-Pacific face a bigger definitional dilemma. They were originally forged to deter the USSR. The threat to the alliance partners today is from an assertive China, which they are reluctant to define as a strategic adversary, because of their economic engagement with it and the huge military asymmetry.
Geography link
It is often overlooked that geostrategy derives from both geography and politics. While politics is dynamic, geography is immutable. Two major imperatives flow from India’s geography: economic and security interests in the Indo-Pacific space and the strategic importance of the continental landmass to its north and west. The former has inspired the Act East policy of bilateral and multilateral engagements in Southeast Asia and East Asia and the Pacific. Shared India-U.S. interests in dealing with the challenge from China in the maritime domain have been a strategic underpinning of the bilateral partnership since the early 2000s.
In the immediate-term, Indian and U.S. perspectives are less convergent in India’s continental neighbourhood. Connectivity and cooperation with Afghanistan and Central Asia need engagement with Iran and Russia, as well as with the Russia-China dynamics in the region. Russia bestrides the Eurasian landmass bordering India’s near and extended neighbourhood. Seemingly paradoxically, a close Russia-China partnership should move India to broad-base relations with Russia (beyond the traditional defence and energy pillars). A strong stake in relations with India could reinforce Russia’s reluctance (which still persists) to be a junior partner of China.
As the U.S. confronts the challenge to its dominance from China, classical balance of power considerations would dictate a modicum of accommodation with Russia. There was an analogous logic in the Richard Nixon-Henry Kissinger outreach to China in 1971, when the Soviet Union was the more formidable rival. The political lessons from the current pandemic could help reawaken that historical memory. Equally, the U.S. could acknowledge that India’s development of trade routes through Iran would also serve its strategic interest of finding routes to Afghanistan and Central Asia, bypassing Pakistan and Russia, respectively.
A template and UNSC term
Five years ago, a group of U.S. strategic analysts had suggested (in a report for the Council on Foreign Relations), that the U.S. should see ties with India as a joint venture (not an alliance), in which they could pursue shared objectives to mutual benefit and accept that differences of perspectives will have to be addressed.
This template could have wider applicability for bilateral relations in today’s world order, which former National Security Adviser Shivshankar Menon has described as militarily unipolar, economically multipolar and politically confused. COVID-19 may scramble the economics and deepen the confusion further.
India will acquire a larger global profile next year, when it commences a two-year term on the UN Security Council. The strategic choices that it makes in its bilateral partnerships will be closely watched.
Date:09-09-20
Mountains that sustain millions
Outsiders have dissociated the Himalayas from the people and the people from the resources
Juno Negi is Junior Research Fellow at the Wildlife Institute of India, Dehradun
The word Himalaya comes from two Sanskrit words: Him (snow) and Aalay (abode). The beauty of the Himalaya, which are one of the youngest chains of mountains in the world harbouring a diverse ecosystem, lies in its intriguing complexity. The region is among the 36 world biodiversity hotspots. According to a report by the International Centre for Integrated Mountain Development, the region encompassing the Hindu Kush Himalaya encompasses 240 million people.
Several challenges
The mountains are the most resilient; yet, ironically, their inhabitants are vulnerable. With few livelihood options, forests form an essential life support system for the locals. However, dwindling natural resources, unsustainable agricultural practices, lack of basic amenities and so on create a challenge for local sustenance. Demographic shifts, weak institutional capacity, poor infrastructure, and a paucity of adequate information on mountain-specific climate change pose challenges to capacity-building in the region.
Studies have revealed low food availability and decreased self-sufficiency owing to the combined pressures of increasing wildlife attacks on crops and livestock and persistent youth out-migration. An increase in male out-migration has put the brunt of household responsibility on the women and the elderly, who tend to focus more labour on livestock production, often to the neglect of crop agriculture, further rendering the land unproductive and prone to wildlife foraging. Lack of irrigation sources and drying up of local gadhera (small river tributaries), dhara (spring), naula (aquifer) etc. amidst uneven precipitation and erratic rainfall have added to the water woes of the hills. With traditional crops being replaced by cash crops, agro-biodiversity of the region has declined and dietary patterns have altered. This has increased nutritional insecurity, and undermined long-term agricultural sustainability in the region.
In the light of such events, what is the role of the government, policymakers, locals and outsiders?
Mountain-specific policies to strengthen livelihood opportunities based on both farm and non-farm activities should be developed. Organic farming methods like use of biopesticides and botanicals and bio-composting should be promoted. Local food systems need to be revived and niche products of the mountain need to be developed. Marketing systems and infrastructure need to be strengthened. Healthy livestock management practices should be explored and the potential of medicinal plants harnessed. Region-specific water security and cleaner energy solutions should be sought by bringing key stakeholders in a synergistic partnership. In all this, people’s role, especially that of the women, should not be ignored. As custodians of important traditional knowledge on preparation of seeds, harvesting, the medicinal use of plant species, etc., their inclusion in policymaking and the decision-making process becomes all the more crucial.
Sacred and sublime
In 2014, the Uttarakhand government declared September 9 as Himalaya Diwas to spread the message of conservation of the Himalayan ecosystems. For those living in the mountain ranges, the word ‘Himalaya’ might not be what they associate themselves with. For them, it is their pahad (mountain), jal (water), jungle, jameen (land), jeev-jantu (living beings), jadi-booti (roots and herbs), roji-roti (daily earnings). We as outsiders have dissociated the mountains from the people, the people from the resources, the resources from their livelihood.
As we come across Himalaya Diwas posters and policy framework documents being released, rallies being carried out and slogans of ‘Himalaya Bachao’ lost amid the grunting of JCB excavators, we should take a moment to reflect on the importance of the mountain system in its entirety. As author Stephen Alter put it, we need to view the Himalaya as both the sacred and the sublime.
चीन पाक की तरह ईरान को भी मोहरा बनाना चाहता है
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )
पिछले हफ्ते भारतीय विदेश नीति के हिसाब से दो घटनाएं अचानक हुईं, लेकिन वे दोनों ही महत्वपूर्ण रहीं। पहली, भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की चीनी रक्षामंत्री वेई फेंग्हे से भेंट और दूसरी, तेहरान रुककर ईरान के रक्षामंत्री से उनकी भेंट। ये दोनों घटनाएं पूर्व-नियोजित और सुनिश्चित नहीं थीं, लेकिन इनके परिणाम भारतीय विदेश नीति की दृष्टि से सार्थक हो सकते हैं। ध्यान देने लायक बात यह है कि जब राजनाथ के मास्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने की खबर छपी तो विदेश मंत्रालय ने साफ-साफ कहा कि हमारे रक्षामंत्री चीन के रक्षामंत्री से वहां बात नहीं करेंगे। लेकिन बात हुई और दो घंटे हुई। चीनी रक्षामंत्री फेंग्हे ने तीन बार अनुरोध किया कि वे भारत के रक्षामंत्री से मिलना चाहते हैं और वे खुद चलकर उनके होटल आए। चीन के इस शिष्टाचार का एक कारण यह भी हो सकता है कि भारत ने पिछले एक-डेढ़ हफ्ते में पेंगौंग झील के दक्षिण में चुशूल क्षेत्र की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। चीन को यह संदेश पहुंच चुका है कि भारत दबने वाला नहीं है।
दोनों रक्षामंत्रियों ने अपनी-अपनी सरकार के पहले से जाहिर रवैयों को जरूर दोहराया। लेकिन सारे मामलों को बातचीत से सुलझाने की पेशकश की। भारत के सैनिकों का बलिदान हुआ है और भारत में प्रतिशोध का भाव बढ़ा हुआ है। इसके बावजूद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी बात सलीके से पेश की। चीनी रक्षामंत्री और साथ बैठे उनके अफसरों पर इस बात का काफी असर हुआ कि राजनाथ जी ने दोनों देशों के बीच शांति के लिए चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की ऐतिहासिक उक्ति उद्धृत की। शायद इसी का परिणाम है कि अगले दो-तीन दिन में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की मॉस्को में चीनी विदेश मंत्री से भेंट होगी।
चीनी रक्षामंत्री का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में ऊंचा स्थान है और राजनाथ भी मोदी मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ हैं। वे भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी तरह वेई फेंग्हे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नजदीकी माने जाते हैं। अब तक हमारे विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चीनी नेताओं से कई बार बात कर चुके हैं लेकिन मास्को में हुए उक्त संवाद का असर कुछ बेहतर ही होगा। यह असंभव नहीं, जैसा कि मैं शुरु से कह रहा हूं, कि अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिन फिंग के बीच संपूर्ण भारत-चीन सीमांत को पक्का करने पर सीधी बात हो सकती है। यह ठीक है कि भारत-चीन, दोनों की जनता आवेश में है लेकिन दोनों देशों के नेता जानते हैं कि सीमांत पर युद्ध हुआ तो दोनों के लिए 1962 से भी ज्यादा विनाशकारी होगा। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने अभी तक कोई भी उत्तेजक बात नहीं कही है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि भारत चीनी अतिक्रमण को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा। भारत की सैन्य-तैयारी में कोई कमी नहीं है।
सैन्य-तैयारी के साथ-साथ कूटनीतिक मुस्तैदी भी भारत पूरी तरह दिखा रहा है। हमारे रक्षामंत्री का अचानक ईरान पहुंच जाना आखिर किस बात का सबूत है? इधर चीन ने ईरान के साथ जबरदस्त पींगें बढ़ाई हैं। एक-डेढ़ माह पहले दुनिया को पता चला कि चीन अब ईरान में 400 अरब डॉलर की पूंजी लगाएगा। अगले 25 साल में होनेवाले इस चीनी विनियोग का लक्ष्य क्या है? ईरान को भी पाकिस्तान की तरह अपना मोहरा बना लेना। वह ईरान में सड़कें, रेलें, बंदरगाह, स्कूल और हॉस्पिटल बनाएगा। ईरानी फौज को वह प्रशिक्षण, हथियार, जासूसी-सूचना आदि में सहयोग देगा। उसका लक्ष्य है, अमेरिका और उसके मित्रों इजराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के खिलाफ मोर्चाबंदी करना। चीन फिर अमेरिका के विरोधियों- फिलस्तीन, सीरिया और तुर्की आदि को भी हवा देना चाहेगा। आजकल अमेरिका चीन का जितना विरोधी हो रहा है, उससे भी ज्यादा वह ईरान का है। ट्रम्प प्रशासन ने परमाणु मसले को लेकर ईरान पर दोबारा प्रतिबंध थोप दिए हैं। चीन इसी का फायदा उठाना चाहता है।
यह चीनी कूटनीतिक चक्रव्यूह भारत के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है, हालांकि प्रकट रूप से ऐसा कहा नहीं जा रहा। भारत ने ईरान के चाहबहार बंदरगाह और चाहबहार-जाहिदान सड़क बनाने का जो जिम्मा लिया हुआ है, वह खटाई में पड़ सकता है। मध्य एशिया के पांचों राष्ट्रों से ईरान के जरिए आवागमन की व्यवस्था अधर में लटक सकती है। अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत ने जो जरंज-दिलाराम सड़क बनाई थी, चीन चाहेगा कि भारत उसके उपयोग से वंचित हो जाए। पाक का वर्चस्व बढ़ाने के लिए चीन तालिबान की पीठ भी ठोक सकता है। चीन चाहेगा कि शिया ईरान और सुन्नी पाकिस्तान में कोई सांठ-गांठ हो जाए। हमारे रक्षामंत्री की यह ईरान यात्रा इन्हीं सब आशंकाओं के निराकरण की दृष्टि से हुई है। ईरान के संबंध अमेरिका से बहुत खराब हैं और आजकल भारत से अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं। इसके बावजूद भारत के रक्षामंत्री और विदेश मंत्री ईरानी नेताओं से बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? क्या यह नहीं कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है। वह अपने राष्ट्रहितों की रक्षा को सर्वोपरि समझता है।
Date:09-09-20
अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ हिंदी अकेले नहीं लड़ सकती
योगेन्द्र यादव, ( सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इंडिया )
इस साल हिंदी दिवस (14 सितंबर) पर हिंदी भाषियों, हिंदी प्रेमियों और शुभचिंतकों को पांच संकल्प लेने चाहिए ताकि हमें राजभाषा पखवाड़े के पाखंड से मुक्ति मिले। साथ ही हिंदी दिवस के नाम पर हर साल हिंदी की बरसी न मनानी पड़े। कड़वा सच यह है कि अंग्रेजों के जाने के बाद से देश में अंग्रेजी की गुलामी घटी नहीं, बढ़ी है। एक दिन हिंदी दिवस है, बाकी 364 दिन अघोषित अंग्रेजी दिवस। सच यह है कि ‘राजभाषा’ नामक कागज का गहना पहनी सरकारी हिंदी की हैसियत स्वामिनी की नहीं, सेविका जैसी है। जैसे मालकिन से झाड़ खाने के बाद दासी घर में बच्चों पर हाथ चलाती है, मालकिन से मिली साड़ी पहन पड़ोसन पर ऐंठ दिखाती है। वैसे ही हिंदी बाकी भारतीय भाषाओं पर झूठा रौब जमाती है। अपनी ही दर्जनों बोलियों का गला दबाती है। संख्या के हिसाब से दुनिया की चौथी बड़ी भाषा बोलने वाले इससे पिंड छुड़ाने आतुर हैं।
सरकारी नीति का सच यह है कि नई शिक्षा नीति के बहाने मातृभाषा में शिक्षा पर भले सार्थक बहस हुई हो, लेकिन जब एक तमिल राजनेता ने हिंदी वर्चस्व का खतरा बताया तो सरकार ने तुरंत सफाई दी कि हिंदी लादने की कोई मंशा नहीं है। यानी अंग्रेजी के वर्चस्व को कोई खतरा नहीं है। सच यह है कि न पिछली सरकारों में हिम्मत थी और न ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दुहाई देने वाली इस सरकार में यह हिम्मत है कि वह सत्ता और बाजार में अंग्रेजी के वर्चस्व को हाथ भी लगा सके।
सच यह है कि अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई अकेली हिंदी लड़ नहीं सकती। जब तक सभी भारतीय भाषाएं एक-दूसरे का हाथ नहीं पकड़तीं, यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हिंदी को विशेष अधिकार नहीं बल्कि विशेष जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वह सभी भारतीय भाषाओं को जोड़े। यह तभी संभव होगा अगर हिंदी छोटी मालकिन बनने का लालच छोड़, बाकी भारतीय भाषाओं की सास और खुद अपनी बोलियों की सौतेली मां बनने की बजाय उनकी सहेली बने। हिंदी देश की सभी भाषाओं के बीच पुल का काम कर सकती है, लेकिन तभी अगर वह खुद इसकी मांग न करे, बस बाकियों को अपने ऊपर से आने-जाने का मौका दे, अगर वह अपने भीतर हिंद देश की विविधता को आत्मसात कर पाए।
पहला संकल्प: हम हिंदी की पूजा-अर्चना करने की बजाय उसका इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ घर और रसोई में ही नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा के मंचों पर हिंदी बोलेंगे, सोशल मीडिया पर हिंदी भी लिखेंगे। बचपन के संस्मरण को याद करने के लिए ही नहीं, देश-दुनिया के भविष्य की बात भी हिंदी में करेंगे। सिर्फ बुजुर्गों से नहीं, बच्चों से भी हिंदी में बात करेंगे, उन्हें हिंदी सिखाएंगे।
दूसरा संकल्प: हम हिंदी के शिल्पियों को मान देंगे, हिंदी के बाजार को पैसा देंगे। सिर्फ हिंदी के सीरियल देखने या क्रिकेट या राजनीति की कमेंट्री हिंदी में सुनने से भाषा नहीं बचेगी। भाषा तभी बचती है जब शब्द बचते हैं, गढ़े जाते हैं, साहित्य रचा जाता है, ज्ञान का निर्माण होता है। इसलिए ड्राइंग रूम में हिंदी का अखबार रखेंगे, बच्चों को बर्थडे गिफ्ट में हिंदी की किताबें भेंट करेंगे, असमिया और मलयालियों से सीखेंगे कि साहित्यकारों का सम्मान कैसे किया जाता है। हिंदी में बाल और किशोर साहित्य तथा विज्ञान रचना के लिए अनेक अवॉर्ड देंगे।
तीसरा संकल्प: हम शुद्ध हिंदी का आग्रह त्याग देंगे, हिंदी को अलग-अलग स्वर और व्याकरण में सुनने-पढ़ने की आदत डालेंगे। हिंदी तभी बड़ी बन सकती है जब वह बड़ा दिल रखे: आकाशवाणी की सरकारी हिंदी के साथ मुंबइया हिंदी, उर्दू से घुली-मिली हिंदी भी चलेगी, तो दर्जनों बोलियों में रंगी हिंदी भी। कबीर और रैदास की पुरानी हिंदी को समझेंगे तो साथ में ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र को अपनी नई हिंदी का आविष्कार करना होगा।
चौथा संकल्प: हर हिंदी भाषी एक गैर हिंदी भारतीय भाषा सीखेगा। रवींद्रनाथ ठाकुर, सुब्रह्मण्यम भारती, अमृता प्रीतम, कुवेंपु या नामदेव धसाल को मूल में पढ़ने से हिंदी भी समृद्ध होगी। तीसरी भाषा के नाम पर रट्टामार संस्कृत की खानापूर्ति की बजाय अगर उत्तर प्रदेश में तमिल, बिहार में बांग्ला, हरियाणा में तेलुगू, राजस्थान में कन्नड़, मध्यप्रदेश में मराठी और छत्तीसगढ़ में ओड़िआ सिखाई जाए तो हिंदी द्वेष अपने आप खत्म हो जाएगा।
पांचवां संकल्प: ‘राष्ट्रभाषा’ शब्द का इस्तेमाल हम हिंदीभाषी भूलकर भी नहीं करेंगे। संविधान या कोई भी कानून देश में किसी भी एक ‘राष्ट्रभाषा’ का जिक्र नहीं करता। बेहतर हो कि हिंदी ‘राजभाषा’ का कागजी आभूषण वापस कर दे। हिंदी के प्रचार-प्रसार का काम सरकार न करे। अगर महात्मा गांधी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सरीखा कोई गैर-हिंदी भाषी हिंदी के गुणगान करना चाहे तो उसकी मर्जी, हिंदी भाषी खुद यह काम छोड़ दें। 14 सितंबर को हिंदी दिवस की जगह भारतीय भाषाओं का ‘भाषा दिवस’ मनाया जाए। अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़ने का राष्ट्रीय आंदोलन तभी सफल होगा जिस दिन भारत में भारत की भाषाओं को किसी एक दिवस की जरूरत ही न रहे।
हालात बिगाड़ता चीन
संपादकीय
लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना की आक्रामक हरकतें जिस तरह बढ़ती जा रही हैं उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि चीन कपट के साथ उन्माद से भी ग्रस्त हो गया है। उसकी सेना सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश भी कर रही है और यह ढोंग भी कर रही कि वह संयम का परिचय दे रही है। विगत दिवस उसकी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर न केवल हवाई फायरिंग करती दिखी, बल्कि लोहे की छड़ें लिए हुए भी नजर आई। वह इससे बौखलाई हुई है कि भारतीय सेना ने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया और कुछ उन चोटियों पर कब्जा कर लिया जिन पर उसकी नजर थी। चूंकि चीनी सेना की हरकतों से यह साफ है कि चीनी नेतृत्व उसे उकसा रहा है, इसलिए भारत को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए न केवल तैयार रहना होगा, बल्कि यह भी प्रदर्शित करना होगा कि वह अपने कदम पीछे खींचने वाला नहीं है। इसके लिए उसे अपनी सैन्य तैयारियों में तेजी लानी होगी। यह तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि टकराव की स्थिति में चीन भारतीय सेना की मारक क्षमता का अनुमान भी न लगा सके। इसके साथ ही लद्दाख में चीन की आक्रामकता का जवाब अन्य मोर्चे पर देने के विकल्प भी खुले रखे जाने चाहिए। ये विकल्प हिंद महासागर में भी खुले रखे जाने चाहिए, जहां से बड़ी संख्या में चीनी मालवाहक जहाज गुजरते हैं।
चीन को न केवल यह संदेश जाना चाहिए कि उसकी सैन्य शरारत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, बल्कि यह भी कि उसकी तमाम बौखलाहट और गीदड़ भभकियों के बावजूद भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर बातचीत के जरिये समस्या का समाधान करने को तैयार है। यह संदेश विश्व समुदाय को भी दिया जाना चाहिए, ताकि उसका ध्यान चीन की बदनीयती की ओर खींचा जा सके। बातचीत के जरिये समस्या समाधान की प्रतिबद्धता जताने के साथ-साथ चीन के समक्ष यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि उसका यह स्वांग चलने वाला नहीं कि उसके कब्जे वाली जमीन तो उसकी और शेष पर बातचीत संभव है। चीन के साथ कोई भी बातचीत उसकी शर्तों पर कदापि नहीं होनी चाहिए। चीन को दबाव में लेने के लिए अब यह भी आवश्यक हो गया है कि भारत उसके कब्जे वाले अपने इलाकों को लेकर अपना दावा नए सिरे से रेखांकित करे। इसी तरह, यदि चीन अरुणाचल प्रदेश को भारतीय हिस्सा मानने से इन्कार करता है तो भारत के लिए भी यह सर्वथा उचित होगा कि वह तिब्बत पर चीन के कब्जे को अवैध बताने में संकोच न करे। कपटी चीन की संवेदनाओं को महत्व देने का अब कोई मतलब नहीं।
![]() Date:09-09-20
Date:09-09-20
संकटग्रस्त संपत्ति का निस्तारण
संपादकीय
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उस विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है जिसका गठन कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए बैंक ऋण के निस्तारण के वित्तीय मानक सुझाने के लिए किया गया था। वरिष्ठ बैंकर के वी कामत की अध्यक्षता वाली समिति ने 26 क्षेत्रों में ऐसे ऋण से निपटने के लिए एक खाका सुझाया है। यह असाधारण स्थिति है जहां सरकार द्वारा महामारी को थामने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन ने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही कंपनियों की राजस्व और कर्ज चुकाने की क्षमता को प्रभावित किया। ऐसी स्थिति में यह महत्त्वपूर्ण हो गया कि बेहतर संचालन वाली कंपनियों की मदद की जाए और अनावश्यक दिवालिया होने की घटनाओं को रोका जाए। क्योंकि ये घटनाएं बैंकिंग तंत्र को प्रभावित करेंगी। इस संदर्भ में समिति की अनुशंसाएं तार्किक प्रतीत होती हैं और इनके माध्यम से हालात से निपटने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। निस्तारण कंपनियों के वित्तीय मानकों पर निर्भर करेगा। मिसाल के तौर पर समायोजित कुल शुद्ध मूल्य में बाहरी देनदारी की हिस्सेदारी, चालू अनुपात, डेट सर्विस कवरेज रेशियो और ब्याज, कर, अवमूल्यन और परिशोधन पूर्व आय में ऋण की हिस्सेदारी।
समिति ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सीमा की अनुशंसा भी की है। इसके अलावा केवल वही खाते राहत के लायक होंगे जो 1 मार्च तक मानक खाते के रूप में वर्गीकृत थे और जिनका बकाया 30 दिन से कम का था। इसके अलावा निस्तारण प्रक्रिया वर्ष के अंत के पहले शुरू करनी होगी।
ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि राहत केवल महामारी के असर को कम करने तक सीमित रहे। इसके अतिरिक्त नियामक के मुताबिक इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट जैसी अन्य जरूरी अनिवार्यताएं एवं मानक भी इसके तहत लागू होंगे। चूंकि बैंकों को तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का शीघ्र निस्तारण करना होगा इसलिए कुछ आवश्यकताओं के चलते प्रक्रिया में देरी हो सकती है। एक ओर जहां पैनल की अनुशंसाओं और नियामक द्वारा अपनाए गए ढांचे में सुरक्षा उपाय हैं वहीं इसके बावजूद यह सुनिश्चित करना अहम होगा कि यह सुविधा फंसे हुए कर्ज को छिपाने के लिए नहीं इस्तेमाल की जाए। देश में नियामकीय सहनशीलता के उदाहरण बहुत उत्साहित करने वाले नहीं हैं। हालांकि अल्पावधि में ऐसा धैर्य अधिकांश अंशधारकों के हित में होता है लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती।
इसके अलावा कुछ अन्य मसले हैं जिन पर नीतिगत तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए समिति ने ध्यान दिया कि बैंकिंग क्षेत्र के विश्लेषण में शामिल करीब 72 फीसदी कर्ज महामारी से प्रभावित है। यह समझना आवश्यक है कि कॉर्पोरेट और बैंकों की बैलेंस शीट दोनों कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के पहले से ही तनावग्रस्त थीं। महामारी ने हालात और खराब कर दिए। विश्लेषकों का कहना है कि बड़ी तादाद में ऐसी फर्म भी हैं जो नई व्यवस्था के तहत निस्तारण के काबिल नहीं होंगी। यह स्पष्ट नहीं है कि बैंक अल्पावधि में ऐसी कंपनियों से कैसे निपटेंगे। व्यवस्था में व्याप्त तनाव को देखते हुए फंसे हुए कर्ज में जबरदस्त इजाफा लाजिमी है।
ऐसे में आरबीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि फंसा हुआ कर्ज समय पर चिह्नित हो और बैंकिंग तंत्र के पास पर्याप्त पूंजी हो। इस परिदृश्य में जहां निजी क्षेत्र के बैंक पूंजी एकत्रित कर रहे हैं, वहीं यह स्पष्ट नहीं है कि सरकारी बैंकों के पूंजीकरण की क्या योजना है। कमजोर बैंकिंग तंत्र ऋण को प्रभावित करेगा और आर्थिक सुधार की गति पर भी असर होगा। यानी स्थायी सुधार इस बात पर निर्भर है कि हम महामारी को कितनी जल्दी थाम पाते हैं। लगातार बढ़ता संक्रमण सुधार को प्रभावित करेगा और व्यवस्था में तनाव बढ़ेगा।
महिला सबलीकरण की हकीकत
ज्योति सिडाना
हमारे समाज में पुरुष-सत्ता के मूल्यों के आधार पर महिलाओं का समाजीकरण कुछ इस तरह से किया जाता रहा है कि महिला के अस्तित्व को पुरुष से अलग करके देखा ही नहीं जाता। महिलाओं के जीवन से जुड़ा हर निर्णय पुरुष-सत्ता ही तय करती आई है। यह भी एक तथ्य है कि लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन लैंगिक भेदभाव का ही एक उदाहरण है। इसी प्रकार पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री के यौन संबंधी कार्य भी पुरुषों की मर्जी से निर्धारित होते रहे हैं। कुछ नारीवादी विचारक मानते हैं कि स्वतंत्र प्रजनन और यौन कर्म के लिए शोषण को खत्म करना जरूरी है। यह तभी हो सकता है जब पूंजीवादी व्यवस्था और पितृसत्ता का अंत हो।
स्त्री को नियंत्रित करने के लिए पुरुष हमेशा से ‘भय के मनोविज्ञान’ का प्रयोग करता रहा है, जैसे कभी परिवार की मर्यादा के नाम पर, कभी उसे शारीरिक और बौद्धिक कमजोरी का यकीन दिला कर, मासिक धर्म के समय उसकी पवित्रता को संदेहास्पद मान कर, पति की सेवा को उसका धर्म और जन्म-मरण से मुक्ति का मार्ग बता कर या फिर संतान उत्पन्न न होने पर उसे मोक्ष न मिलने का तर्क देकर स्त्री को सदा अधीन बनाए रखता है। समाज में इसी तरह की अनेक किवदंतियां और पूर्वाग्रह लंबे समय से चले आ रहे हैं। विडंबना है कि शिक्षित और आधुनिक समाज भी आज तक इन रूढ़ियों पर अंकुश नहीं लगा पाया या कहें कि लगाना ही नहीं चाहता।
ऐसा देखते आए हैं कि विवाह के समय लड़की की उम्र लड़के से कम होनी चहिए, क्यों? शायद कम उम्र की लड़की में परिपक्वता कम होने के कारण उसको नियंत्रित-निर्देशित करना तुलनात्मक रूप से सरल होता है और उसका समाजीकरण मनमाने तरीके से किया जा सकता है। ऐसे में महिला समाजीकरण और उसका सबलीकरण विरोधाभासी नजर आते हैं। अगर महिलाओं का समाजीकरण पुरुष-सत्ता के अंतर्गत हुआ है, तो उसके सबलीकरण की बात ही बेमानी हो जाती है। अन्यथा महिला आरक्षण को अब तक लोकसभा में स्वीकृति मिल गई होती। क्या महिलाओं का सबलीकरण पुरुष समाज के समक्ष अनेक चुनौतियों को उत्पन्न करता है, जिसके भय से महिलाओं के आरक्षण विधेयक को पास नहीं होने दिया गया। यह एक ऐसा अनुत्तरित प्रश्न है, जिस पर विमर्श करने से भी शायद लोग कतराते हैं। महिलाओं के संदर्भ में ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जिन पर विमर्श या सार्वजानिक चर्चा करने की जरूर सदियों से अनुभव की जाती रही है, पर समाज, राज्य, अकादमिक जगत और बुद्धिजीवी सभी खामोश हैं।
कुछ समय पहले महिला सुरक्षा को लेकर सत्ता के गलियारों में कुछ चर्चा सुनाई दी, पर परिणाम हम सबके सामने है। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो महिला सुरक्षा को लेकर लोगों का गुस्सा कुछ देर के लिए दिखने लगता है, पर कुछ समय बाद वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। लड़कियों को देर रात या सांझ के बाद घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए, उन्हें छोटे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, उन्हें लड़कों की बराबरी नहीं करनी चाहिए, उन्हें ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए जोर-जोर से नहीं हंसना चाहिए, सड़क चलते लड़कों की फब्ती पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, आदि। आखिर ऐसा क्यों? क्यों किया जाता है महिलाओं का ऐसा समाजीकरण? पशु और स्त्री में क्या कोई फर्क नहीं है? या यह मान लिया गया है कि स्त्री के पास केवल शरीर होता है, मस्तिष्क नहीं? वह केवल भावनात्मक प्राणी है, इसलिए बौद्धिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से उसे वंचित रखने का प्रयास जारी है? क्या महिला आरक्षण विधेयक का पास न हो पाना वास्तव में महिलाओं के विशिष्ट समाजीकरण और उसकी पुरुष द्वारा की गई व्याख्या में निहित हैं? देखा जाए तो महिलाओं के सबलीकरण के यथार्थ को उनके समाजीकरण की विसंगतियों के आधार पर ही समझा जा सकता है। इस समाजीकरण में महिलाओं के शरीर, पवित्रता-अपवित्रता के संदर्भ, महिलाओं द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे प्रतीक (विवाह पूर्व, विवाहित, विधवा के रूप में), बच्चों के जन्म तथा पालन-पोषण, रसोई में उनकी भूमिका, ससुराल और पति के बारे में दृष्टिकोण, भाषा के प्रयोग, विभिन्न व्यवसायों से जुड़ी महिलाओं, यौन संबंधों के सवाल, पोशाक, भोजन संबंधी आदतों आदि के बारे में बताते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? चाहे वे घरेलू महिलाएं हों या पेशे से जुड़ी, सभी महिलाओं का समाजीकरण ऐसे ही किया जाता है और इन्हें सभ्यता और संस्कृति की व्याख्या का भाग बनाया जाता है, क्योंकि इन्हें सहेजने की जिम्मेदारी महिला को सौंपी गई है। अगर ये सभी व्याख्याएं और निर्धारण पुरुष करे तो सबलीकरण कैसा?
अभी कुछ समय पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक पति द्वारा दायर तलाक याचिका के मामले में कहा कि अगर विवाहिता हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार मंगलसूत्र, चूड़ियां और सिंदूर लगाने से इनकार करती है, तो यह माना जाएगा कि विवाहिता को शादी अस्वीकार है। यह किस तरह का तर्क है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इस तरह का कोई तर्क नहीं दिया गया है कि पत्नी द्वारा इन प्रतीकों का प्रयोग न करने पर विवाह को अवैध माना जाएगा। तो फिर इस निर्णय का आधार क्या है? दूसरा उदाहरण, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था। वर्ष 2005 में संशोधन के बाद उन्हें यह अधिकार मिला, पर इस शर्त के साथ कि यह अधिकार केवल 2005 के बाद जन्मी पुत्रियों को होगा। वर्ष 2015 में पुन: इस निर्णय को संशोधित किया गया और सभी पुत्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया, जिसे अनेक चुनौतियों के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दी है। स्त्री को अपने किसी भी अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष क्यों करना पड़ता है? शिक्षा का अधिकार, बराबरी का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, नौकरी करने या न करने का अधिकार, संतान पैदा करने या न करने का अधिकार, विवाह करने या अविवाहित रहने का अधिकार, यहां तक कि अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार, अपना भविष्य तय करने का अधिकार, क्या ये सब अधिकार महिलाओं के व्यक्तित्व का हिस्सा बन पाए हैं। अगर नहीं तो फिर कैसा सबलीकरण? इन सभी सवालों पर ‘महिलाओं की आलोचना’ या ‘महिलाओं का संकोच’ उनके अराजनीतिक और असंगठित होने का सबूत कहा जा सकता है। महिलाओं की स्वतंत्रता, उदारता, समानता और खुलेपन को परिवार और समाज-विरोधी मान लिया जाता है। इसलिए सिमेन द बोउआ तर्क देती हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र परिवेश से पृथक रखा जाता है और ‘निर्भरता से जीवन में संतुष्टि मिलती है’, का विचार महिला की चेतना का हिस्सा बना दिया जाता है। परिवार, पति, बच्चे, कपड़े, रसोई पर तो उसे चर्चा करने का हक है, पर इस दायरे के बाहर का विश्व उसके चिंतन का विषय क्षेत्र नहीं हो सकता। पुरुष समाज ने हमेशा महिला को अधीनस्थ बनाया है, जिसे समाप्त किए बिना महिला सबलीकरण का रास्ता तलाशना कठिन है।
वर्तमान दौर में ‘ज्ञान शक्ति है’ का तर्क यह संकेत देता है कि महिला को भी ज्ञान के क्षेत्र में इतना गहरे उतरना होगा कि वह न केवल हर तरह के भय का सामना कर सके, बल्कि इस सभ्य कहे जाने वाले समाज में एक शिष्ट जीवन भी जी सके। ज्ञान की इस शक्ति द्वारा ही महिला न केवल अपने शोषण से मुक्ति पा सकती है, बल्कि शक्ति संबंधों में भी अपना स्थान सुनिश्चित कर सकती है और तभी बराबरी का समाज उभार ले सकता है।
रोबोट से है बड़ा खतरा
डॉ. जयंतीलाल भंडारी
यदि हम भारत में रोबोट तैनाती का परिदृश्य देखें तो पाते हैं कि देश में वाहन उद्योग में रोबोटों की संख्या सबसे अधिक है। रोबोट की तैनाती का वाहन उद्योग में रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा रहा है। जैसे-जैसे दुनिया में रोबोट बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे भारत सहित दुनिया के अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों में रोजगार की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं।
दुनिया की अर्थव्यवस्था में रोबोट की अहमियत कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाज अमेरिका के बोस्टन कंसल्टीन ग्रुप की रिपोर्ट 2019 से लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार रोबोट का वैश्विक बाजार छलांगे लगाकर बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2010 में दुनिया में रोबोट का बाजार करीब 15 अरब डॉलर मूल्य का था। यह 2020 में करीब 43 अरब डॉलर का हो गया है और अनुमान है कि 2025 तक 67 अरब डॉलर का हो जाएगा। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा कार्यरत रोबोट जिन देशों के पास है, उनमें चीन, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा जर्मनी प्रमुख हैं। दुनिया में विभिन्न प्रकार के रोबोटों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। सामान्यतया रोबोट दो तरह के होते हैं-इंडस्ट्रीयल रोबोट और सर्विस रोबोट इंडस्ट्रीयल रोबोट औद्योगिक एवं कारोबार इकाइयों में काम करते हैं, जबकि सर्विस रोबोट सर्विस से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं।
सर्विस रोबोट के तहत प्रोफेशनल्स रोबोट, डोमेस्टिक सर्विस रोबोट, इंटरटेनमेंट रोबोट शामिल होते है। दुनिया में रोबोटों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर प्रसिद्ध र्वल्ड रोबोटिक्स 2019 की एक्जीक्यूटिव समरी महत्त्वपूर्ण है। इसके अनुसार दुनिया में आपरेशनल स्टॉक में याने कार्यरत इंडस्ट्रीयल रोबोट की संख्या जो 2018 में करीब 24 लाख थी, यह 2022 में बढ़कर करीब 40 लाख होने का अनुमान है। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि इंडस्ट्रीयल रोबोट चीन में सर्वाधिक हैं। वर्ष 2018 में चीन में करीब 6.5 लाख इंडस्ट्रीयल रोबोट का स्टॉक था। चीन में प्रत्येक 10,000 कर्मचारियों पर 732 रोबोट काम कर रहे हैं। हमारे देश में रोबोटों की संख्या के मद्देनजर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स 2019 की रिपोर्ट उल्लेखनीय है। इसके मुताबिक भारत में 2018 में करीब 23 हजार इंडस्ट्रीयल रोबोट कार्यरत थे। पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीयल रोबोट्स के मामले में भारत 11वें स्थान पर है। भारत में वर्ष 2018 में करीब 4771 नये इंडस्ट्रीयल रोबोट लगाए गए थे। यह संख्या 2020 के अंत तक छह हजार होने की संभावना बताई गई है। भारत में औद्योगिक सेक्टर में हर 10,000 कर्मचारियों पर चार रोबोट काम कर रहे हैं। यदि हम भारत में रोबोट तैनाती का परिदृश्य देखें तो पाते हैं कि देश में वाहन उद्योग में रोबोटों की संख्या सबसे अधिक है। रोबोट की तैनाती का वाहन उद्योग में रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा रहा है। निश्चित रूप से कोविड-19 के बाद दुनिया में उपभोक्ताओं की प्राथमिकता में रोबोट की अहमियत और बढ़ेंगी।
जहां एक ओर रोबोट वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा हो जाएंगे और जिन देशों में कार्यशील युवाओं की कमी है उन देशों में रोबोट अत्यधिक लाभप्रद होंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर जिन देशों में आबादी अधिक है और कार्यशील युवाओं की अधिकता है, उन देशों में रोबोट के बढ़ने से रोजगार व नौकरियां जाने की चिंताएं बढ़ेंगी। निसंदेह रोबोट से नौकरियां खोने का चिंताजनक परिदृश्य भारत में अधिक दिखाई देगा। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रोजगार रहित विकास नामक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में तेजी से रोजगार के दरवाजे पर दस्तक देने वाले युवाओं की संख्या को देखते हुए हर साल करीब 81 लाख नई नौकरियां और नए रोजगार अवसर पैदा करने की जरूरत है। ऐसे में इतने रोजगार के अवसर और नौकरियां जुटाने के लिए भारत को 18 फीसद विकास दर की जरूरत होगी। ऐसे में छलांगे लगाकर बढ़ रही नौकरियों की जरूरतों के बीच देश में रोबोटों की तैनाती चुनौतीपूर्ण होगी। हाल ही में 26 अगस्त को मैकिंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट (एमजीआई) ने ‘इंडियाज टर्निंग प्वाइंट-एन इकोनॉमिक एजेंडा टु स्पर ग्रोथ ऐंड जॉब’ नाम से जारी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 2029-30 तक गैर कृषि नौकरियों की तलाश में 9 करोड़ अतिरिक्त लोग निकलेंगे।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड के बाद 2029-30 तक हर साल 1.2 करोड़ गैर कृषि नौकरियों की सालाना जरूरत होगी, जबकि वर्ष 2012 और 2018 के बीच हर साल महज 40 लाख नौकरियों का ही सृजन हो सका है। ऐसे में जहां बड़े पैमाने पर नई नौकरियां सृजित की जाना होगी वहीं देश में बढ़ते हुए रोबोट व ऑटोमेशन मशीनों के चलते नौकरियों में कमी आने की भी बड़ी चुनौती होगी। देश में रोबोट के बढ़ने से डाटा एंट्री क्लर्क, फैक्टरी मजदूर, बिजनेस सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, अकाउंटेंट, जनरल ऑपरेशन मैनेजर, स्टॉक कीपिंग क्लर्क, डाक सेवा क्लर्क, वित्तीय समीक्षक, कैशियर व टिकट क्लर्क, मैकेनिक, बिजली व टेलीकॉम रिपेयर सेवा, बैंक क्लर्क, कार, वैन और मोटरसाइकिल चालक, एजेंट व ब्रोकर, घर-घर सामान बेचने का काम, वकील, बीमा क्लर्क और वेंडर सर्विस जैसे सेक्टर में नौकरियां कम होंगी, लेकिन हमें रोबोटिक्स की बढ़ती हुई वैश्विक उपयोगिता के बीच देश की विकास नीति में रोबोट की भूमिका पर भी विशेष विचार मंथन अवश्य करना होगा। चूंकि देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रतिस्पर्धा वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है। अतएव जब दुनिया रोबोट के इस्तेमाल की ओर बढ़ रही है तो देश के मैन्युफैक्चरर उससे बहुत दूरी बनाकर नहीं रह सकते हैं।
आईटी जैसे क्षेत्रों में भी रोबोट के महत्त्व से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में रोबोट की उपयोगिता और देश में रोजगार की राह देख रही नई पीढ़ी की आकांक्षाओं के बीच उपयुक्त तालमेल करते हुए देश में रोबोटों की उपयुक्त संख्या में तैनाती का निर्धारण किया जाना होगा। ऐसे में जहां एक ओर देश में जरूरी क्षेत्रों में उपयुक्त संख्या में रोबोट का उपयोग किया जाए, वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा रोबोट से बढ़ती रोजगार चिंताओं पर ध्यान देते हुए देश की नई पीढ़ी को रोबोट जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उच्च कौशल से प्रशिक्षित करने की नई रणनीति बनाई जाए।
Date:09-09-20
संजीदा हो सरकार
ज्ञानेन्द्र रावत
आज देश के भाल हिमालय का समूचा क्षेत्र संकट में है। इसका प्रमुख कारण इस समूचे क्षेत्र में विकास के नाम पर अंधाधुंध बन रहे अनगिनत बांध, पर्यटन के नाम पर हिमालय को चीर कर बनाई जा रही ऑल वैदर रोड और उससे जुड़ी सड़कें हैं। दुख इस बात का है कि हमारे नीति-नियंताओं ने कभी भी इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचा तक नहीं। वे आंख बंद कर इस क्षेत्र में पनबिजली परियोजनाओं को और पर्यटन को ही विकास का प्रतीक मानकर उनको स्वीकृति-दर-स्वीकृति प्रदान करते रहे हैं, बिना यह जाने-समझे कि इससे पारिस्थितिकी तंत्र को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा।
पर्यावरण प्रभावित होगा वह अलग जिसकी भरपायी असंभव होगी। विडम्बना यह है कि यह सब उस स्थिति में हो रहा है, जबकि दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित कर दिया है कि बांध पर्यावरण के लिए भीषण खतरा हैं और दुनिया के दूसरे देश अपने यहां से धीरे-धीरे बांधों को कम करते जा रहे हैं। इसके लिए किसी एक सरकार को दोष देना मुनासिब नहीं होगा। वह चाहे संप्रग सरकार हो या फिर राजग, दोनों में कोई फर्क नहीं है।
जहां तक संप्रग सरकार का सवाल है तो उसने पर्यावरणविदों और गंगा की अस्मिता की रक्षा के लिए किये जा रहे आंदोलनकारियों के दबाव में उत्तराखण्ड में बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी थी, लेकिन 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद राजग सरकार ने न केवल बांधों के निर्माण को मंजूरी दी बल्कि इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास की खातिर पहाड़ों को काट-काटकर सड़कों के निर्माण को मंजूरी और दे दी। अब सवाल यह है कि यदि यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो इस पूरे हिमालयी क्षेत्र का पर्यावरण कैसे बचेगा। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि हमारी सरकार और देश के नीति-नियंता, योजनाकार यह कदापि नहीं सोचते-विचारते कि हिमालय पूरे देश का दायित्व है। वह देश का भाल है, गौरव है, स्वाभिमान है, प्राण है। जीवन के सारे आधार यथा-जल, वायु, मृदा सभी हिमालय की देन हैं। देश की तकरीब 65 फीसद आबादी का आधार हिमालय ही है क्योंकि उसी के प्रताप से वह फलीभूत होती है। और यदि उसी हिमालय की पारिस्थितिकी प्रभावित होती है तो देा प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। ऐसे हालात में जरूरत इस बात की है और वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और समाजविज्ञानी सभी मानते हैं कि हिमालय की सुरक्षा के लिए सरकार को इस क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र के विकास के मौजूदा मॉडल को बदलना होगा। उसे बांधों के विस्तार की नीति भी बदलनी होगी। साथ ही पर्यटन के नाम पर सड़कों के लिए पहाड़ों के विना को भी रोकना होगा। क्येंकि बांधों से नदियां तो सूखती ही हैं, इसके पारिस्थितिकीय खतरों से निपटना भी आसान नहीं होता। यदि एक बार नदियां सूखने लगती हैं तो फिर वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पहाड़ जो हमारी हरित संपदा और पारिस्थितिकी में अहम भूमिका निभाहते हैं, नहीं होंगे तो हमारा वष्रा चक्र प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा, परिणामत: मानव अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। एक समय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा था कि, ‘हिमालय को प्रदूषण से बचाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए काम करने की महती आवश्यकता है। कारण हिमालय पर पारिस्थितिकी का खतरा बढ़ गया है। इस स्थिति में हिमालय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना सबसे बड़ी सेवा है।’
विडम्बना यह कि इस बात को सरकार और उसके समर्थक मानने को कतई तैयार नहीं हैं। लगता है वे विकास के फोबिया से ग्रस्त हैं। उन्हें न पर्यावरण की चिंता है, न मानव जीवन की। इसी स्वार्थी प्रवृत्ति ने हिमालय का सर्वनाश किया। वह चाहे हिमालय के उत्तर-पूर्व हों या पश्चिमी राज्य। हिमालय से निकली नदियों की हमारे देश में हरित और श्वेत क्रांति में महती भूमिका है। इन्हीं नदियों पर बने बांध देश की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन विडम्बना कि उसी हिमालय क्षेत्र के तकरीब 40 से 50 फीसद गांव आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।
यही नहीं तकरीब 60-65 फीसदी देा के लोगों की प्यास बुझाने वाला हिमालय अपने ही लोगों की प्यास बुझाने में असमर्थ है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सत्ता प्रतिष्ठान इस हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिकी की वजहों के हल तलाशें और ऐसे विकास को तरजीह दें जिनसे पर्यावरण की बुनियाद मजबूत हो। तभी कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।
चीनी पैंतरों से सावधान
संपादकीय
मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग की मुलाकात के बाद जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के मिलने की योजना सामने आई, तब ऐसा लगा था कि बीजिंग शायद जमीनी हकीकत को तस्लीम करना चाहता है, और अब उच्च स्तरीय बातचीत का रास्ता खुलने से स्थितियां बेहतरी की ओर बढ़ेंगी। हालांकि, तब भी त्वरित समाधान की उम्मीद किसी ने नहीं बांधी थी। लेकिन विदेश मंत्रियों की बैठक से ठीक पहले उसकी फौज ने पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से एक बार फिर उकसाने वाली कार्रवाई की है, उससे तो यह साफ हो गया है कि बीजिंग की दिलचस्पी विवाद सुलझाने में नहीं, बल्कि भारत को उलझाए रखने में है। इसीलिए उसने प्रॉपगैंडा का सहारा लेते हुए इस बार भारत पर ही ‘वॉर्निंग शॉट्स’ दागने का आरोप लगाया है। लेकिन उसकी पैंतरेबाजी को अब दुनिया समझ चुकी है, और उसकी विश्वसनीयता का संकट तो इतना गहरा चुका है कि कम से कम भारत से जुड़े मामलों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी वह अलग-थलग पड़ने लगा है।
ताजा घटनाक्रमों के बारे में भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि चीनी सैनिक ‘फॉरवर्ड पोजिशन’ के करीब आने की कोशिश कर रहे थे और जब दिलेर भारतीय जवानों ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी, तो उन्होंने डराने के लिए हवा में गोलियां दागीं। भारतीय सेना तो शुरू से ही एलएसी पर शांति और विश्वास बहाली के प्रति प्रतिबद्ध रही है, लेकिन अपने देश की संप्रभुता और अखंडता से वह कोई समझौता नहीं करेगी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गलवान घाटी की 15 जून की घटना के बाद से अब तक उद्धत रवैया अपनाए हुए है। लेकिन बीजिंग को यह समझना होगा कि इस तनावपूर्ण स्थिति की कीमत उसे भी चुकानी होगी। कुछ कदम तो भारत सरकार उठा भी चुकी है और कुछ अन्य सख्त कदमों के लिए उस पर जन-दबाव बढ़ता जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ कर दिया है कि सरहदी मुल्कों के रिश्ते सीमा से निरपेक्ष नहीं होते। इसलिए अब तय बीजिंग को करना है।
कई दशकों से भारत समग्र सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू करने की अपील करता रहा है, लेकिन भयादोहन की अपनी पारंपरिक कूटनीति के तहत बीजिंग इसे हल नहीं करना चाहता। पूर्वी लद्दाख की कुचेष्टाएं उसकी मंशा बता रही हैं। वह जानता है कि एक बार सीमा-निर्धारण हो गया, तो भारत अब इतना समर्थ हो चुका है कि उसकी सरहदों पर वह कोई मनमानी नहीं कर पाएगा। फिलहाल हमारी चुनौती यह है कि हमें कोरोना महामारी से भी जंग लड़नी है, गिरती अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी जूझना है और भौगोलिक सरहदों की हिफाजत के लिए भी तैयार रहना है। यह देश के लिए परीक्षा की घड़़ी है। एक नागरिक के स्तर पर भी और नेतृत्व के स्तर पर भी। दुर्योग से ऐसे मौकों पर जो राजनीतिक एकजुटता दिखनी चाहिए, वह बहुत मुखर नहीं है। सरकार को विदेश नीति के मसले पर समूचे विपक्ष को भरोसे में लेकर रणनीति बनानी चाहिए, ताकि सामूहिक प्रतिबद्धता के समवेत स्वर सरहद पार पहुंचें। ये स्वर विरोधी सत्ता प्रतिष्ठानों के मनोविज्ञान को तो छूते ही हैं, देश के भीतर भी नया आत्मविश्वास भरते हैं। बीजिंग की पैंतरेबाजी और प्रॉपगैंडा का जवाब भी इसी में है। भारत को अब उससे सीमा पर ही नहीं, सोच के मैदान में भी निपटना है।
Date:09-09-20
हिमालय से भी क्यों बड़ा हो गया हमारा स्वार्थ
ज्ञानेन्द्र रावत, वरिष्ठ पत्रकार व पर्यावरणविद
हिमालय की रक्षा का सवाल हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। इसमें दो राय नहीं कि यदि हिमालय न होता, तो हमारा अस्तित्व ही न होता। यह हमारे जीवन का आधार है, लेकिन आज इसके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। इस संदर्भ में बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिक अनिल वी कुलकर्णी की मानें, तो हिमालय पर आसन्न संकट से हम बेखबर हैं। इसके ग्लेशियर जिस तेजी से पिघल रहे हैं, वह हमारे लिए कम चिंतनीय नहीं है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलाव की दर में 1984 से 2012 के बीच जो अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वह खतरनाक संकेत है। हिमालय के चंद्रा बेसिन के इन ग्लेश्यिरों के पिघलने की यही रफ्तार जारी रही, तो हमारी प्रमुख नदियों के सूखने का खतरा बढ़ जाएगा और नदियों के बिना इस भूभाग में मानव अस्तित्व की कल्पना बेमानी होगी। वैज्ञानिक कुलकर्णी ने यह चेतावनी एनल्ज ऑफ ग्लेश्यिोलॉजी में प्रकाशित अपने शोध पत्र में देते हुए कहा है कि ग्लेश्यिरों का पिघलना इसी तरह जारी रहा, तो झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा। हिमालयी क्षेत्र की नदियों की जलधाराओं की क्षीण होती स्थिति इस चेतावनी की जीती-जागती मिसाल है। इसमें मानवीय दखलंदाजी ने अहम भूमिका निभाई है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता।
जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि के भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ग्लेश्यिरों के पिघलने के अलावा हिमालयी क्षेत्र में मिलने वाली शंखपुष्पी, जटामासी, पृष्पवर्णी, गिलोय, सर्पगंधा, पुतली, अनीस, जंबू, उतीस, भोजपत्र, फर्न, गेली, तुमड़ी, वनपलास, कुनेर, टाकिल, पाम, तानसेन, अमार, गौंत, गेठी, चमखड़िक और विजासाल जैसी प्रजातियों और जीवों की चिरू जैसी असंख्य प्रजातियों के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। यदि अब भी नहीं चेते, तो असंख्य प्रजातियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। यदि संयुक्त राष्ट्र की मानें, तो अगले 100 वर्ष में 20 प्रतिशत प्रजातियां सदा-सदा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। आज वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और समाज विज्ञानी मानते हैं कि हिमालय की सुरक्षा के लिए सरकार को इस क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र के विकास के मौजूदा मॉडल को बदलना होगा।
दरअसल, आज देश के भाल हिमालय पर संकट का प्रमुख कारण इस समूचे क्षेत्र में विकास के नाम पर अंधाधुंध बन रहे अनगिनत बांध, पर्यटन के नाम पर हिमालय को चीरकर बनाई जा रही ऑल वैदर रोड और उससे जुड़ी सड़कें हैं। दुख इस बात का है कि हमारे नीति-नियंताओं ने कभी इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचा तक नहीं, जबकि दुनिया के दूसरे देश अपने यहां से धीरे-धीरे बांधों को कम करते जा रहे हैं। सवाल यह है कि यदि यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा, तो इस पूरे हिमालयी क्षेत्र का पर्यावरण कैसे बचेगा? देश की करीब 65 फीसदी आबादी का आधार हिमालय ही है। यदि हिमालय की पारिस्थितिकी प्रभावित होती है, तो देश प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। इसीलिए सरकार को बांधों के विस्तार की नीति बदलनी होगी और पर्यटन के नाम पर पहाड़ों के विनाश को भी रोकना होगा। बांधों से नदियां तो सूखती ही हैं, इसके खतरों से निपटना भी आसान नहीं होता। यदि एक बार नदियां सूखने लगती हैं, तो फिर वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। पहाड़ जो हमारी हरित संपदा और पारिस्थितिकी में अहम भूमिका निभाते हैं, अगर नहीं होंगे, तो हमारा वर्षा चक्र प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा।
आज जिस तरह की नीतियां चल रही हैं, उनके अनुसार, नदी मात्र जल की बहती धारा है और पर्यटन आर्थिक लाभ का साधन। योजनाकारों ने हिमालय से निकलने वाली नदी को बस बिजली पैदा करने का स्रोत मान लिया है। हमारा स्वार्थ हिमालय से भी बड़ा हो गया है। स्वार्थी प्रवृत्ति ने ही हिमालय को खतरे में डाल दिया है। इसी सोच के चलते हिमालय के अंग-भंग होने का सिलसिला और उसकी तबाही जारी है। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि यह पूरा क्षेत्र भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है। यहां निर्माण, विस्फोट, सुरंग, सड़क का जाल बिछने से पहाड़ तो खंड-खंड होते ही हैं, वहां रहने वालों के घर भी तबाह होते हैं। समग्र समावेशी विकास नीति बनाए बिना हिमालय को बचाना मुश्किल है।
