
08-06-2022 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:08-06-22
Date:08-06-22
Look At Per Capita
Environment reports don’t do justice to better measure of India’s carbon footprint.
TOI Editorials

Reports such as EPI need to be seen in the light of two aspects. One, almost one in six humans live in India. Two, India’s cumulative CO2 emissions till 2019 were a mere 3% as against 47% of the US and EU combined. In other words, the earliest to industrialise have emitted most of the greenhouse gases (GHG) and some of them also happen to be the best EPI performers. Given this context, India fares quite well in per capita terms. To illustrate, GHG intensity of growth rate is a measure of progress in decoupling emissions from economic growth. India ranks 34, while the US and Germany are at 44 and 48 respectively.
Similarly, in terms of per capita GHG emission, India is at 53 and ahead of Norway. EPI’s data set shows India’s economic rise has come with a smaller environmental footprint. If this is to continue, access to cutting-edge technology is essential. Therefore, it’s in everyone’s interest to craft a mechanism to make technology widely accessible. India’s per capita energy consumption in 2019 for air-conditioning was just 25% of the world average of 272 kWh. This gap will narrow with growth and its environmental impact can be disproportionately smaller with the newest technology.
EPI also shows that India’s performance on air quality is abysmal. That’s why GoI promulgated an ordinance in 2020 as it needed immediate attention. Pollution Control Board data shows that poor air quality is mainly on account of post-harvest practices in agriculture and natural causes. Their solutions lie within. For instance, not all farmers burn stubble to clear fields. Where stubble has an economic value and hence a market, it is not burnt. Governments can compress coordination timelines to link farmers to a relevant market. Cost-effective solutions to reduce the impact of natural causes such as dust need attention right away. Finally, rethinking the role of public transport is indispensable.
Date:08-06-22
Indigenise Smart
Heavy investment in R&D is needed to take Indian defence production to next level.
TOI Editorials
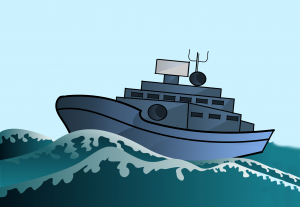
Plus, the performance of Russian military platforms in the war has been poor, with a large number of armoured fighting vehicles breaking down. Thus, India has to get out of this position where its foreign policy is constricted and a large part of its military arsenal may not deliver desired results. That said, indigenisation has to be done smartly. For the proposed construction of the eight indigenous corvettes, an Indian shipyard will be selected through competitive bidding. Unless tightly controlled, the bidding process could throw up controversies that defeat long-term objectives.
Additionally, while India has achieved 90% indigenisation in the ‘float’ (hull and superstructure) component of warship-building, the ‘move’ (propulsion) and ‘fight’ (weapons) components lag behind at 60% and 50% indigenisation respectively. Similarly, we are still far off from developing a fully indigenous aero-engine for military aircraft with the old Kaveri project having failed to meet standards. Overall, most of our indigenisation success has been in auxiliary and spares. But to take indigenisation to the next level we need to significantly up our investment in R&D and create a cutting-edge military-industrial ecosystem with universities, private sector and defence PSUs working in tandem. That in turn requires the Indian economy to grow at a high, sustained rate.
हिंदू-मुस्लिम दोराहे पर ठहर गया है देश
मिन्हाज मर्चेंट, ( लेखक, प्रकाशक और सम्पादक )
हर देश के इतिहास में ऐसा क्षण आता है, जब उसे जटिल विषयों की आंखों में आंखें डालकर देखना होता है। भारत में हिंदू-मुस्लिम टकराव अब उसी स्थिति में आ गया है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत ने विवेकशीलता का परिचय देते हुए जुलाई तक सुनवाई को टाल दिया है। गर्मियां खत्म हो चुकी होंगी और शायद इस मामले का तापमान भी तब तक कम हो जाए।
अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में सर्वोच्च अदालत के निर्णय से उत्साहित हिंदू समूहों ने मुगलों और अन्य आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए गए दूसरे मंदिरों पर दावा पेश कर दिया है। अब मनाली में भी मंदिर-मस्जिद विवाद नागरिक अदालत में चला गया है। हमें कहीं न कहीं लक्ष्मणरेखा खींचनी होगी, नहीं तो हम अपना अगला दशक स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे पर चर्चा करने के बजाय मंदिर-मस्जिद पर बहस करते हुए बिता देंगे। मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं को भी अधिक समावेशी होना पड़ेगा। अभी तो वे मुगलों की परम्परा के समर्थक मालूम होते हैं। ताली दोनों हाथों से ही बजती है। मुस्लिमों के धर्मगुरुओं को हिंदुओं के साथ एक सहमति बनानी चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग तोड़े गए प्रमुख मंदिरों के पुनर्निर्माण में मदद कर सकते हैं। बदले में हिंदू भी यह आश्वासन दें कि अब वे इस तरह की और मांगें नहीं करेंगे और रोजमर्रा के सामान्य जीवन की बहाली में व्यस्त हो जाएंगे।
उस तरह का समझौता अभी भले दूर का सपना लगे, लेकिन अदालतें इसकी निगरानी कर सकती हैं। पूजास्थल कानून 1991 को एक मानदण्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कानून कहता है कि ‘कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या समुदाय के पूजास्थल को उसी धर्म के किसी दूसरे समुदाय या किसी भी समुदाय के दूसरे धर्म के पूजास्थल में नहीं बदल सकता है।’ नवम्बर 2020 में राम मंदिर मामले में सर्वोच्च अदालत के निर्णय को भी एक अन्य नजीर माना जा सकता है। उस निर्णय में संतुलन बनाने वाले केंद्रीय तत्व पर ध्यान दें : ‘22-23 दिसम्बर 1949 को बाबरी मस्जिद से मुस्लिमों का आधिपत्य समाप्त हो गया था, जिसे 6 दिसम्बर 1992 को ध्वस्त कर दिया गया। अदालत को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बुरा हुआ है, उसका निदान करे। अगर अदालत इस तथ्य की अनदेखी करेगी कि अनुचित तरीके से मुस्लिमों को मस्जिद पर उनके अधिकार से वंचित किया गया था तो यह न्यायपूर्ण नहीं होगा।’
वहीं भारत के कानून आयोग के पूर्व सदस्य ताहिर महमूद कहते हैं, ‘अगर काशी और मथुरा विवादों पर देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाता है तो शांति और सौहार्द के पक्ष में किसी भी अदालती आदेश पर आपत्तियां नहीं ली जानी चाहिए।’
जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब राम मंदिर बीजेपी का बड़ा एजेंडा था। वहीं कांग्रेस, सपा, राजद, एनसीपी आदि जैसी सेकुलर पार्टियां मुस्लिम-फर्स्ट की नीति का पालन करती थीं। वास्तव में उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मोदी 2019 में भी चुनाव जीत जाएंगे। नवम्बर-दिसम्बर 2018 में राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में मिली जीत से कांग्रेस को यकीन हो गया था कि मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे। जनवरी 2019 में ओपिनियन पोल भी यही बता रहे थे कि भाजपा के हाथ से देश के लोगों का समर्थन फिसल रहा है। कांग्रेस के अंदरूनी थिंक टैंक का अनुमान था कि आम चुनाव में कांग्रेस 170 सीटें जीतेगी और 2004 की तरह गठबंधन सरकार बनाने में सफल रहेगी। कांग्रेस के अंदरूनी लोग तो आत्मविश्वास से यूपीए-3 की बात करने लगे थे।
लेकिन पुलवामा ने सब बदल दिया। फरवरी 2019 में जैशे-मोहम्मद के इस आतंकी हमले के बाद भारत ने बालाकोट में पलटवार किया, जिसने चुनावी समीकरणों को बदल दिया। जनवरी 2019 में प्रकाशित मेरे एक सर्वेक्षण में भाजपा को 220-230 सीटें मिलने का पूर्वानुमान लगाया गया था। बालाकोट के बाद मैंने एक और विश्लेषण किया, जो मार्च 2019 में प्रकाशित हुआ। इसमें अब भाजपा को 270 और एनडीए को 300 सीटें मिलने की बात कही गई थी। लेकिन अंत में भाजपा खुद 300 से ज्यादा सीटें जीत गई। इससे कांग्रेस स्तब्ध थी। तभी से वह हिंदू-मुस्लिम मसले को उठाए हुए है और भाजपा भी यही कर रही है। नतीजा यह है कि आज देश जितना ध्रुवीकृत हो गया है, उतना पहले कभी नहीं था। भारत में दशकों से साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे। आज उतने बड़े पैमाने पर तो दंगे नहीं होते, लेकिन मुस्लिमों के प्रति विद्वेष बढ़ा है और मध्यवर्गीय पेशेवर हिंदुओं में भी यह प्रवृत्ति विकसित होती दिख रही है।
जो हिंदू पांच साल पहले तक लिबरल थे, वे भी अब मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा अतीत में किए अन्यायों पर मुखर होकर बोलने लगे हैं। मुस्लिमों ने प्रतिक्रिया में खुद को सेकुलर पार्टियों की जकड़बंदी में और फंसा लिया है, जो उन्हें 1947 से ही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से बंधक बनाए हैं। जबकि उन्हें अलगाव की भावना को त्यागकर भारतीयता की भावना को अंगीकार करना होगा। अदालतों को भी मंदिरों और मस्जिदों सम्बंधी याचिकाओं पर लक्ष्मणरेखा खींचना होगी। सर्वोच्च अदालत वैसी सभी याचिकाओं को मिलाकर किसी ऐसे नतीजे पर पहुंच सकती है, जो देश के विकास में बाधक बनने के बजाय उसमें सहयोगी बने।
 Date:08-06-22
Date:08-06-22
स्थायी हल
संपादकीय
भारत और चीन समेत करीब 60 देशों ने जिनेवा में 12 जून से होने जा रही विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की 12वीं मंत्रिस्तरीय शिखर बैठक में विचार के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव खाद्य भंडारण, कृषि सब्सिडी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और मानवीय सहायता से जुड़े कुछ विवादित मसलों को हल करने पर केंद्रित है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दुनिया के सामने गंभीर खाद्यान्न संकट है और वह उसका स्थायी हल तलाशने की कोशिश में है। इस पहल के लिए बने समूह के घटक इसे महत्त्वपूर्ण बनाते हैं क्योंकि इसमें एशिया, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र के खाद्य निर्यातक ही नहीं बल्कि आयातक देश भी हैं। इनमें भारत, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान तथा कई अन्य देश शामिल हैं। इन देशों ने सुझाव दिया है कि कृषि सब्सिडी के आकलन का उन्नत और संशोधित तरीका अपनाया जाए।
सन 1986-88 की कीमतों को मानक मानकर इन सब्सिडी का आकलन करने की मौजूदा प्रणाली अब पुरानी तथा अप्रासंगिक हो चुकी है। इसी प्रकार अनुमति योग्य सब्सिडी से संबंधित मौजूदा प्रावधानों, जो अधिकतम कुल उपज मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित हैं, उन पर तथा सब्सिडी की इस सीमा का उल्लंघन होने पर पैदा होने वाले विवादों को दूर रखने के लिए बने ‘शांति संबंधी प्रावधान’ पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित संशोधनों के लिए डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते को लगभग नए तरीके से तैयार करना होगा। यह समझौता 1994 में हुआ था लेकिन यह व्यापार गतिरोध समाप्त करने, पारदर्शी बाजार पहुंच सुनिश्चित करने तथा एकीकृत वैश्विक बाजार तैयार करने जैसे अपने तय लक्ष्य हासिल करने में विफल रहा। भारत लंबे समय से इस समझौते की आलोचना करता रहा है। उसका कहना है कि यह समझौता विकसित देशों की ओर झुका हुआ है। अब जबकि भारत को कम से कम 59 देशों का समर्थन हासिल है, खासकर जब उसके पास चीन जैसे प्रभावशाली देशों का समर्थन भी है तो शायद वह इस समझौते को समकालीन हकीकतों के अनुरूप बनाने तथा सभी को समान अवसर देने की बात पर जोर दे सकता है।
दरअसल इस समझौते को तैयार करने तथा इस पर हुई वार्ता में अमेरिका और यूरोपीय संघ प्रमुख भूमिका में थे। सन 1990 के दशक के आरंभ में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स ऐंड ट्रेड (गैट) वार्ता में भी इनका ही दबदबा था। विकासशील देशों के वार्ताकारों में आमतौर पर उनके व्यापार मंत्रालयों के अधिकारी हुआ करते थे और वे कृषि तथा किसानों से जुड़े मुद्दों से बहुत परिचित भी नहीं थे। इन वार्ताओं में उन्हें ज्यादा वजन से अपनी बात भी नहीं रखने दी गई। आश्चर्य नहीं कि उस दौरान सारे नियम विकसित देशों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से बनाए गए, न कि खाद्य पदार्थों की कमी से जूझ रहे विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को हल करने के लिए। यहां तक कि सब्सिडी के आकलन के लिए निर्धारित 1986-88 की संदर्भ अवधि भी अमीर देशों के अनुकूल है क्योंकि इससे उन्हें अपने किसानों की मदद का अवसर मिलता है जबकि विकासशील देशों के किसान ऐसी मदद से वंचित रह जाते हैं।
इन 60 देशों द्वारा प्रस्तावित नयी योजना में सब्सिडी की संदर्भ कीमतों के आकलन के वर्ष को 1986-88 के बजाय अधिक नवीन मसलन बीते पांच वर्ष की कीमतों के अनुरूप (इस दौर की उच्चतम और न्यूनतम कीमत को छोड़कर) करने की बात शामिल है। इसमें खाद्यान्न संकट से जूझ रहे देशों की मदद के लिए सरकारी भंडार के अनाज के सशर्त निर्यात की इजाजत की मांग भी की गई है। विकासशील देशों को खाद्यान्न उत्पादन, अधिग्रहण तथा भंडारण संबंधी नीतियां बनाने में अधिक लचीलापन देने की बात भी इसमें शामिल है। ऐसा करते हुए घरेलू खाद्य सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस कदम का लक्ष्य है डब्ल्यूटीओ के मानकों को आधुनिक बनाना ताकि दुनिया भर के किसानों और उपभोक्ताओं के हितों का बचाव करते हुए वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
आसान नहीं शांति की राह
संजीव पांडेय
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दस महीने बाद संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई है, वह चिंता पैदा करने वाली है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अफगानिस्तान के भीतर अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियां बेखौफ जारी हैं। इससे क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार अलकायदा के करीब चार सौ लड़ाके अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में मौजूद हैं और इनमें ज्यादातर लड़ाके पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमा के हैं। जाहिर है, आइएस वहां भाड़े के लड़ाके तैयार कर रहा है। इसके अलावा लश्कर और जैश के भी आतंकी प्रशिक्षण केंद्र वहां चल रहे हैं। अफगानिस्तान की धरती पर अगर यह सब हो रहा है तो बिना तालिबान सरकार की सहमति और मदद के यह संभव नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि तालिबान आतंकी संगठनों को पालने-पोसने की नीति पर चल रहा है।
हालांकि अफगानिस्तान को लेकर ईरान, भारत और ताजिकिस्तान सहित अन्य देशों की दुशान्बे में क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद के चौथे दौर की बैठक हुई, लेकिन इसका कोई खास परिणाम सामने नहीं आया। पिछले साल नवंबर में आयोजित पहले क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में पाकिस्तान और चीन की भागीदारी नहीं थी। लेकिन इस बार दुशान्बे में चीन और रूस के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। चूंकि चीन और रूस शुरू से तालिबान सत्ता के समर्थक रहे हैं, इस लिहाज देखा जाए तो दुशान्बे की बैठक का अपना महत्त्व है। दरअसल अफगानिस्तान की शांति में सबसे बड़ी बाधा क्षेत्रीय शक्तियों का आपसी टकराव है। शांति प्रयासों को लेकर क्षेत्रीय विमर्श भले हो रहे हों, लेकिन इसमें भाग लेने वाले देशों के आपसी हितों के टकराव किसी से छिपे नहीं हैं। अफगानिस्तान में अपने हितों के लिए संघर्ष कर रहे भारत, पाकिस्तान और चीन का आपसी टकराव जगजाहिर है। इसी तरह ईरान-पाकिस्तान के बीच गतिरोध भी सामने हैं।
पर जब बात अफगानिस्तान की धरती के आतंकी इस्तेमाल और वहां मौजूद आतंकी संगठनों की गतिविधियों की आती है तो सभी देश अपने हितों को ध्यान में रखते हुए आतंकी संगठनों की पहचान कर उनके खात्मे पर जोर देने लगते हैं। चीन की चिंता अफगानिस्तान की धरती पर मौजूद उइगर आतंकी संगठनों को लेकर है। चीन सिर्फ ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के खिलाफ ही कार्रवाई चाहता है। जबकि भारत की चिंता पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को लेकर है। ये दोनों आतंकी संगठन पाकिस्तान सैन्य प्रतिष्ठान और खुफिया एजंसी आइएसआइ के संरक्षण में काम करते हैं और इनका निशाना केवल भारत है। जबकि पाकिस्तान की चिंता सिर्फ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को लेकर है। यानी हर देश केवल उसी आतंकी संगठन पर लगाम पर जोर देता है जिससे वह खुद परेशान है। चीन और पाकिस्तान जैश और लश्कर पर कार्रवाई को तैयार नहीं है। जबकि अलकायदा से लेकर अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान सत्ता तंत्र के नजदीक हैं। ईरान की अपनी अलग सोच है। पाकिस्तान के नजदीक जो भी आतंकी संगठन होगा, ईरान उसके खिलाफ है। ऐसे में आतंकी संगठनों का खात्मा और शांति की उम्मीद बेमानी लगने लगती है।
पर अब समय की मांग है कि चीन, पाकिस्तान, ईरान जैसे देश अपना नजरिया बदलें। अगर अफगानिस्तान में शांति चाहिए तो वहां मौजूद तमाम आतंकी संगठनों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि अफगान तालिबान के शासन में आतंकी संगठनों की गतिविधियां लगातार जोर पकड़ती जा रही हैं। अमेरिका से हुए शांति समझौते के वक्त अफगान तालिबान ने जो वादा किया था कि वह अपनी धरती से किसी भी आतंकी संगठन को काम नहीं करने देगा, वह झूठा साबित हुआ। देखा जाए तो आतंकी संगठनों पर कार्रवाई को लेकर पश्चिमी ताकतें कभी गंभीर नहीं रहीं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अफगानिस्तान के भीतर अलकायदा, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयब्बा के आतंकियों के मौजूद होने की रिपोर्ट महज खानापूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं लगती। फिर अब तो अमेरिकी फौज भी अफगानिस्तान की जमीन पर नहीं है। जब अफगानिस्तान की जमीन पर अमेरिकी सैनिक थे, तब भी अफगान तालिबान, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर-ए-तैयब्बा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन पूरी ताकत के साथ काम कर रहे थे। अफगान तालिबान के संरक्षण में वहां अफीम की खेती और कारोबार होता ही रहा है और यह अब ज्यादा तेजी से फल-फूल रहा है।
अफगानिस्तान को लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद के ठोस नतीजे नहीं आने का कारण यह भी है कि इसमें अफगानिस्तान के हितों पर गहराई से विचार विमर्श के बजाय जोर सबका अपने-अपने हितों पर ज्यादा रहता है। इस समय काबुल में पाकिस्तान के बिना कोई भी सुरक्षा विमर्श बेमानी है। वैसे तो कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान में नई सरकार सत्ता में आई है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति नहीं हो पाई थी, इसलिए पाकिस्तान बैठक में शामिल नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नजरिया पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से अलग होगा। शहबाज शरीफ बड़े कारोबारी भी हैं और वे क्षेत्रीय शांति का महत्त्व समझते हैं। पर अफगानिस्तान के मामलों में अंतिम फैसला बिना सेना की मर्जी के कर पाना संभव नहीं है। इमरान खान अफगान तालिबान के साथ-साथ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रति भी सहानभूति रखते थे। जबकि टीटीपी के प्रति पाकिस्तानी सेना का नजरिया बिल्कुल अलग है। पाकिस्तानी सेना टीटीपी के साथ किसी भी तरह की बातचीत और समझौते के खिलाफ रही है।
अफगान समाज की कबीलाई मानसिकता को समझे बिना अफगानिस्तान में शांति लाना मुश्किल है। अलकायदा, जैश और लश्कर ने अफगान समाज के कबीलाई विभाजन का जम कर फायदा उठाया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि हाल में तालिबान के मुखिया हबेतुल्लाह अखुंदजाद ने कंधार में एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें तालिबान के लगभग एक सौ अस्सी वरिष्ठ कमांडर शामिल हुए थे। इस बैठक में कंधारी पश्तूनों और हक्कानी नेटवर्क के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। कुछ मुद्दों पर तालिबान के उदारवादी और कट्टर कमांडरों के बीच भी मतभेद दिखे। उदारवादी खेमे के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई जहां दूसरे देशों से अच्छे संबंध विकसित करने वकालत कर रहे थे, वहीं तालिबान के कट्टर कमांडर इससे सहमत नहीं थे। हक्कानी नेटवर्क से जुड़े कमांडर अपना स्वतंत्र वजूद दिखाने में लगे थे। कंधारी पश्तून कमांडरों ने हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी की उपप्रधानमंत्री बनने की कोशिश को नाकाम कर दिया। हक्कानी नेटवर्क आइएसआइ से नियंत्रित होता है जबकि कंधारी तालिबान कमांडर पाकिस्तानी नियंत्रण का विरोध करते रहे हैं।
अफगानिस्तान से सटे और आसपास के देशों को समझना होगा कि इस मुल्क में शांति लाए बिना क्षेत्रीय सहयोग और विकास संभव नहीं होगा। चीन, पाकिस्तान, ईरान सहित सभी देशों की जिम्मेदारी है कि वे अपने निजी हितों का त्याग कर अफगान शांति प्रयासों को आगे बढ़ाएं। साथ ही तालिबान सरकार को भी अपनी जमीन पर आतंकी संगठनों की मौजूदगी खत्म करनी होगी। अगर तालिबान आतंकी संगठनों को मदद और समर्थन की नीति को ही प्राथमिकता देता है तो इसका मतलब यही है वह अफगानिस्तान को और बड़े संकट में झोंक रहा है।
