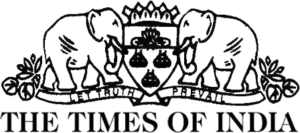05-05-2016 (Important News Clippings)
To Download Click here.
A Taxing Agenda
Data underlines need to widen and deepen tax base, whittle down exemptions and improve compliance.
India’s income tax department released time series data for the period 2000-01 to 2014-15 last week in an attempt to enhance transparency and encourage analysis which could provide insights for policymakers. That’s a good beginning. Some worrying trends in tax collection have been highlighted. And the fact that, in one of the fastest growing countries of the world that is being targeted by most top global wealth management firms, there are just 18,359 individuals who have reported earnings in excess of Rs 1 crore in 2011-12 and paid tax on it. Indeed, by putting in the public domain an annual statement on tax foregone, the government was able to influence public opinion on corporate tax breaks. Similarly, the data on individual tax assessees could help in sensitising many on the need for the affluent to contribute more at a time of growing disparities.
It is disconcerting that of the over five crore individuals who filed their tax returns, 80 per cent of all personal income tax was accounted for by the top 11 per cent, with 1.6 crore tax filers paying no tax — being in the lowest tax bracket. The data also shows that 85 per cent of taxpayers pay less than Rs 1.5 lakh annually — a pointer to the challenges in widening the tax net and raising collections. At first glance, the data on the top earners or the creamy layer — or rather their shockingly low numbers — may further endorse the growing belief of rising income inequality. But if the number of crorepatis appears low, perhaps it may have to do with the fact that a huge chunk of income in the form of long-term capital gains — at Rs 70,121 crore in FY 2012-13, for instance — is exempt from tax. Coupled with that is the set-off of loss in business income (at Rs 67,963 crore) and, to a lesser extent, farm income, which is also not taxed. All this has meant that India’s gross tax to GDP ratio — a key indicator of tax buoyancy but also a wider base — has remained stagnant at close to 10 per cent during the last few years.
For a country like India, which needs to spend on health, education and social security and also build social and physical infrastructure, it is critical to address the challenges on the tax policy front swiftly. These include both the widening and deepening of the tax base, whittling down of exemptions and improving compliance, especially by leveraging technology. The release of data offers an opportunity to policymakers to engage in a wider public debate on the current tax policy, including on the capital gains tax — on which the government has kicked off a corrective step in this year’s budget.
लंबी अवधि में सूखे से निजात के लिए चाहिए नए तरीकों की सौगात
अतीत के अपने अनुभवों से हमने ऐसे कई उपयोगी सबक सीखे हैं जिनको अपनाकर सूखे का प्रबंधन किया जा सकता है। हाल के गंभीर सूखों की बात करें तो वर्ष 2002 और 2009 में आए भीषण सूखे से हम बेहतर तरीके से निपटने में सफल रहे। मौजूदा सूखे से निपटने के बारे में कोई फैसला सुनाना अभी अपरिपक्व कदम होगा। खासतौर पर कुछ राज्यों में देरी से उठाए गए कदमों को देखते हुए। लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्टï है कि जलवायु परिवर्तन के चलते सूखे की आवृत्ति में काफी इजाफा हुआ है लेकिन इसके बावजूद सूखे के प्रभाव में कमी और उससे निपटने की कोशिशों को लेकर भरपूर सराहना का भाव देखने को नहीं मिल सका है। इन पहलुओं पर अधिक जोर से सूखे की गंभीरता को कम करने में मदद मिलती, फसलों का नुकसान कम होता है, पालतू पशुओं से होने वाले उत्पादन की कमी दूर होती है और उन संसाधनों और प्रयासों की रक्षा होती जो अन्यथा राहत कार्यों और सूखा पीडि़त आबादी के पुनर्वास में लगते।
सूखा प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था व्यापक तौर पर सूखा संहिता पर केंद्रित है जिसे पहले अकाल संहिता कहा जाता था। इसे मूलरूप से ब्रिटिश शासकों के दौर में तैयार किया गया था। तब से इसे समय-समय पर संशोधित करके समकालीन जरूरतों के अनुरूप बनाया जाता है। यह संहिता अनिवार्य तौर पर सूखा पीडि़त इलाकों में तदर्थ राहत उपायों मसलन पेयजल मुहैया कराने, खाना, चारा और रोजगार आदि उपलब्ध कराने के इर्दगिर्द घूमती है। एक बार सूखा खत्म होने पर ये उपाय समेट लिए जाते हैं और अगली त्रासदी घटित होने तक किसी का ध्यान उस जगह की ओर नहीं जाता। इस लिहाज से देखा जाए तो मौजूदा संहिता दरअसल समस्या के सामने आने पर उससे निपटने वाली है और इसमें उन उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो लंबी अवधि में सूखे का प्रभाव कम करने में मददगार हो सकते हैं।
इसके लिए अच्छे मौसम की एक संहिता की आवश्यकता होगी जिसमें उन कदमों का जिक्र हो जो सामान्य वर्षा वाले वर्षों में उठाएं जाएं ताकि सूखों से निपटने की दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जा सकें। खासतौर पर उन इलाकों में जहां आमतौर पर अक्सर सूखा पड़ता है या पडऩे की आशंका रहती है। सिंचाई के विस्तार को अक्सर किसी इलाके को सूखे से बचाने का प्राथमिक उपाय माना जाता है। लेकिन यह सूखे की समस्या का पूर्ण निदान नहीं है। तमाम उपलब्ध पानी का प्रयोग करने के बावजूद सूखा प्रभावित इलाके सिंचाई सुविधा से महरूम रह जाएंगे।
हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि देश का कोई भी इलाका सूखे की आशंका से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। सूखे के लिहाज से नवीनतम संवेदनशील प्रांत है असम और पूर्वोत्तर में उसके आसपास का इलाका। यहां चार साल में औसतन एक न एक सूखा आ ही जाता है। सूखे के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील इलाका राजस्थान है जहां सूखा हर ढाई साल में दस्तक देता है। बाकी के इलाकों में यह अवधि अलग-अलग है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश के 13 राज्यों के 185 जिलों के 32.87 करोड़ हेक्टेयर भूभाग में से 12 करोड़ हेक्टेयर भूभाग हर वर्ष सूखे की आशंका से दोचार होता रहता है।
जिन वर्षों में सूखा न पड़ रहा हो उन वर्षों में बारिश के पानी को संरक्षित करना और भंडारित करना सूखे से निपटने की नीति में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। इसका एक तरीका है कृत्रिम जल रिचार्ज ढांचे तैयार करना ताकि बारिश के पानी को सतह के ऊपर के जलाशयों की ओर ले जाया जा सके। इसके साथ ही साथ पानी के बेकार बहने को रोकने के लिए खाली जमीन पर घास आदि लगाई जा सकती है ताकि पानी ठहर सके। इससे मिट्टïी की पकड़ मजबूत होगी और पानी के चलते उसका कटाव बंद होगा। इतना ही नहीं चक बांधों का निर्माण प्राकृतिक जल स्रोतों के आसपास किया जाना चाहिए। इससे न केवल तात्कालिक इस्तेमाल के लिए पानी मिल सकेगा बल्कि उसका रिसाव भी बढिय़ा होगा।
आदर्श स्थिति में बारिश का एक तिहाई हिस्सा तालाबों जैसे सतह पर बने जल संग्रहण ढांचों में रखा जाना चाहिए और शेष दो तिहाई हिस्से को कुंओं और भूजल रिचार्ज के काम में प्रयोग कर लिया जाना चाहिए ताकि संतुलन बरकरार रहे। भूजल रिचार्ज पानी के संरक्षण का सबसे बेहतरीन तरीका है खासतौर पर उन इलाकों में जहां गर्मी बहुत है और सतह पर बने ढांचों से पानी वाष्पित हो जाता है।
ऐसा करने के लिए हमें आधुनिक संरक्षण वाली कृषि तकनीक मसलन जीरो टिलेज यानी बिना हल चलाए सालों साल खेती, मिट्टïी का कटाव रोकने के लिए घासरोपण और अलग ढांचों में फसल उगाने जैसी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा पारंपरिक ज्ञान और बुद्घिमता के आधार पर फसल चक्र तैयार करना होगा। एक से अधिक फसलों की मिश्रित खेती और खेती के साथ गाय और भैंस के बजाय भेड़-बकरी जैसे छोटे पशु पालने चाहिए। ये तमाम कोशिशें सूखे से निपटने में दूरगामी प्रभाव वाली साबित हो सकती हैं।
उत्तराखंड की त्रासदी
कुमाऊं के पुराने लोग एक दंतकथा कहते हैं कि जब बतौर चंद राजाओं की राजधानी शहर अल्मोड़ा बसाया जा रहा था तो स्थपति ने ज्योतिषी से मशवरा कर परंपरानुसार स्थायित्व की कामना के साथ इंद्र के नाम पर क्षेत्र के बीचों बीच एक लोहे की कील गाड़ी। कील की नोंक के शेषनाग का फन छूने पर वह डोला और सतह पर भूकंप आया। स्थपति संतुष्ट हुए कि शेषनाग के फन पर टिकाया गया नगर आगे अक्षय रहेगा, पर राजा तो राजा, हुक्म हुआ कि साबित करो कि कील ने शेषनाग का फन छुआ है। जब कील बाहर खींची गई तो उसकी नोंक पर खून लगा था। इससे राजा तो संतुष्ट हो गए, पर कील दोबारा नहीं गाड़ी जा सकती, यह कहकर ज्योतिषियों और स्थपति ने भविष्यवाणी कर डाली कि यह क्षेत्र अब हमेशा डगमग रहेगा। हम नहीं जानते कि इस दंतकथा में कितनी सच्चाई है, अलबत्ता 2001 में अस्तित्व में आने के पंद्रह बरस बाद भी उत्तराखंड में राजनीतिक डगमगाहट कायम है। प्रांत के लिए संघर्षरत रहा उत्तराखंड क्रांति दल तो पहले ही फूट से बिखर चला था, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी फिर भाजपा की, पर दोनों का एक भी मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और इस अस्थिरता से उत्तराखंडवासियों के सपनों का उत्तराखंड आकार पाने से पहले ही खंड-खंड हो चला।
उत्तर प्रदेश से अलग कर यह राज्य जब बना था तो इसके 70 निर्वाचन क्षेत्रों का पहाड़ी तथा मैदानी भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर क्रमश: 42 और 28 का विभाजन किया गया था। यह उपेक्षित तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के पक्ष में जाता था, लेकिन 2006 के परिसीमन में जनगणना को आधार बनाकर पहाड़ी इलाके के सात निर्वाचन क्षेत्र कम कर दिए गए जिससे पहाड़ बनाम मैदान का विभाजन 36 और 34 का बना। नेताओं के वोट तो खरे हुए, पर उत्तराखंड राज्य के गठन की मूल प्रासंगिकता यानी पहाड़ी इलाकों का कल्याण, खो गई। 65 प्रतिशत भूभाग पर वन से ढके पहाड़ी इलाके में मैदान की तुलना में हमेशा से आबादी कम रही। युवाओं के विस्थापन पर रोक न लगने से जनगणना पर आधारित विभाजन पहाड़ बनाम मैदान के बीच लगातार भेदभाव बढ़ा रहा है। वनों की कटाई तथा प्रतिबंधित क्षेत्र में नियमों के खिलाफ अवैध निर्माण कार्यों ने रही-सही कसर पूरी कर दी। इसी का एक प्रमाण इस समय सूबे के पहाड़ी क्षेत्र के पचास फीसद जंगलों को लपेट में ले चुकी आग है। स्थानीय लोगों के अनुसार सूखे तथा गर्मी का हाथ इस हादसे में उतना नहीं, जितना कि आपदा को दुह कर मुनाफा कमाने के इच्छुक बिल्डरों और अवैध लकड़ी के कारोबारियों और भ्रष्ट अफसरों की तिकड़ी का है।
केदारनाथ में 2013 की विनाशकारी जलप्रलय से तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपनी गद्दी भले ही खोई हो, लेकिन उनके पहले और बाद में भी विकास का पैमाना आर्थिक आधार को बनाकर नाजुक इलाके की गहरी पर्यावरणीय क्षति को नजरअंदाज करना जारी रहा है। अब अगले चुनावों में कोई भी दल सरकार बनाए, यकीन नहीं होता कि धार्मिक या रोमांचक टूरिज्म और पहाड़ी इलाके में भारी भवन निर्माण का भारी लाभ-लोभ त्याग कर पर्यावरण और जनहित की रक्षा को सर्वोपरि मानने वाली नई सरकार विकास के इस विनाशकारी पैमाने को सिरे से बदलना पसंद करेगी। 1965 में जोशीमठ से मलारी के बीच हुए वन विनाश से सबक लेकर 70 के दशक में चंडीप्रसाद भट्ट और गौरादेवी जैसे पर्यावरण प्रेमियों ने इलाके के लोगों को संगठित कर वनों की रक्षा का जो जज्बा जगाया था वह आज कहीं खो गया है और सरकार और स्थानीय लोगों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला इस आग को बुझाने की बजाय भड़का ही अधिक रहा है। क्या यही अनुमान लगाना काफी है कि हादसे में कितने करोड़ की वन संपदा नष्ट हुई? कुदरती वन सरीखी अनमोल देन को सिर्फ रुपयों में तोलना मनुष्य जाति की विनाशकारी भूल है। राज्य की सकल आय बढ़ाने की उतावली जगाकर ही ठेकेदार और बिल्डर अपना खादपानी हर दल की सरकार से पाते और लगातार ताकतवर बनते रहे हैं।
ताज्जुब है कि कोई योजना नहीं बनाता कि अगले साल की जंगल की आग कैसे रोकी जा सकती है अथवा किस तरह स्थानीय जनता को इस आपदा से निपटने का प्रशिक्षण तथा संसाधन मुहैया कराए जा सकते हैं। सरकारों का रुख अभी तो कमोबेश यही दिखता है कि सेना तथा केंद्रीय बल लाकर यह मनहूस आग बुझा दी जाए ताकि गर्मी में आने वाले टूरिस्ट न बिदकें और जान माल की क्षति अगले बरस की चुनावी जीत पर खतरा न बने। यह जानते हुए भी कि स्थानीय लोग, खासकर महिलाएं वनों को बचाने और उनके संवर्धन में कितनी निष्ठा और कामयाबी का प्रदर्शन कर चुकी हैं, गत 15 वर्षों से जंगलों की आग बुझाने का काम (बिना समुचित संसाधनों के) वन विभाग पर ही छोड़ दिया जाता रहा है। जब तक वन विभाग के साथ स्थानीय लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं होते तब तक इस सारे पहाड़ी इलाके को पोसते आए वन नहीं बचाए जा सकते।
याद रखें दुनिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की टंकी माने जाने वाले हिमालयी इलाके के यह प्रकृतिदत्त वन सिर्फ पहाडिय़ों के लिए ही अनमोल नहीं, सारे देश के पर्यावरण के फेफड़े हैं। उनका प्रदूषण और विनाश जारी रहा तो सारे देश के पर्यावरण और जल संसाधनों के लिए भीषण आपदा लाएगा। 1970 के दशक में जब पर्यावरण बचाने के स्वत: स्फूर्त आंदोलन ने उत्तराखंड की आम अनपढ़ महिलाओं को लामबंद कर वनों के विनाशकारी दोहन पर सफलता से रोक लगवाई थी तब वन एवं पर्यावरण नहीं, मात्र वन मंत्रालय हुआ करता था। पर्यावरण संबंधी चिंता उपजने के बाद 1988 में जनता की भागीदारी न्योतने वाली राष्ट्रीय वन नीति बनी। इससे महिलाओं को तो लाभ हुआ ही, साथ ही जंगलों का घनत्व और क्षेत्र भी बढ़ा, पर राज्य बनने के बाद फिर दशा बिगड़ चली। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र से उधार लिए कृषि वानिकी (फार्म फॉरेस्ट्री) सरीखे नारे उछलने लगे, जिनके तहत मैदानी इलाके में विकास के नाम पर वृक्ष आधारित उद्योगों के बड़े कारखाने बने और राज्य सरकारों द्वारा देवभूमि तथा एडवेंचर के लुभावने नारे देकर सस्ते पैकेज टूरिज्म को न्योता गया। इससे प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ी, लेकिन अवैध वन कटान होने लगी। साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्रों तक डीजल की धुआं उगलती गाडिय़ों और लाखों उपभोगवादी नए पर्यटकों की साल भर आवाजाही से सारे पर्यावरण पर घातक घाव लगने लगे। इस उपेक्षा की कीमत आज चुका रहे हैं दूरदराज के वनांचलों में जैसे तैसे जीवनयापन कर रहे प्रांतवासी और हमारे प्रतिनिधि संसद में परस्पर छींटाकशी करते यही गिन रहे हैं कि पेड़ों के जलने से राज्य को कुल कितने रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।
Partner The Private Sector:
PPP is win-win, government cannot deliver universal healthcare on its own .
The highest attainable standard of health is a fundamental right of every human being. In this context, universal access to healthcare assumes prime importance. However, healthcare delivery poses a significant challenge for policymakers in India.
A severe lack of resources means that there is only one doctor per 1,700 citizens in India, well below the minimum ratio of 1:1,000 stipulated by WHO. There are also only 1.3 beds per 1,000 population, significantly lower than other Brics economies and the WHO guideline of 3.5 beds per 1,000 population. In rural areas and smaller towns of India, even basic health services remain inaccessible.
Given the sorry state of affairs it is no surprise that India continues to lag behind poorer neighbours like Bangladesh and Nepal in terms of child mortality. For every 1,000 children born in India between 2011 and 2015, 48 died on average every year before reaching the age of five, according to the World Bank. Equally alarming is the fact that a quarter of the world’s neonatal deaths and 15% of maternal deaths happen in India.
It is pertinent to note here that despite the fairly rapid pace of economic growth that India has experienced in the last 20 years, public health spending in the country is only about 1% of GDP. This compares to 3% in China, 4.1% in Brazil and 8.3% in the US.
Inadequate government spending on healthcare and lack of access to health insurance pushes almost 3% of India’s population into indebtedness and bankruptcy every year. To address this situation, the government needs to come forward and take proactive steps to implement a universal healthcare programme that ensures basic healthcare services for everyone with minimum financial burden being passed on to the patient.
India needs a universal healthcare programme that hinges on affordability and access. This calls for existing public health infrastructure to be revitalised, new medical centres built and modern ICT-based telemedicine technology to be leveraged for addressing the demand-supply gaps in terms of doctors and health facilities. There is an urgent need therefore for public health spending in India to be raised to at least 2.5% of GDP as well as Public Private Partnership (PPP) models in healthcare to be promoted.
The government alone cannot meet the healthcare infrastructure and capacity gaps in Tier II and Tier III cities as well as rural areas. While it’s true that some PPP projects attempted earlier have failed, clear policy guidelines can ensure the successful implementation and sustainability of healthcare PPP models in future.
The prerequisites should include agreed upon scope of work, legal and regulatory framework, resources pooling and management, transparency and accountability, suitable policies and a commitment to public good. It is necessary that PPPs ensure that government services are delivered in an economical, effective and efficient manner.
The role of the government should be proactive and it should identify areas in National Health Programmes, diagnostic and curative services where partnerships are possible. The government should also develop working guidelines based on successful experiences of different states, besides framing quality guidelines with professional help from organisations that already have experience in preparing quality assurance tools. Lastly, smart business models need to be put in place without which it will be difficult for private players to achieve reasonable returns on investment.
It is encouraging to see that the NDA government is looking seriously at PPP models for improving healthcare access to the country’s 1.2 billion people and lessen the healthcare burden on the common man. At a time when the federal government is examining ways to implement healthcare initiatives under the PPP model in a time bound manner, states like Rajasthan have already set the ball rolling.
The Vasundhara Raje government in Rajasthan has partnered with the private sector for running Primary Health Centres (PHCs) and sub-centres across the state. The terms of the PPP engagement are simple. While the state government will provide the necessary infrastructure, medicines, equipment and operational costs, the private operator would provide doctors, paramedics and other staff, free outpatient services and 24-hour emergency services. These PHCs are already reporting encouraging results as the improvement in cleanliness and availability of staff and medicines have led to a jump in the number of patients being treated.
The Rajasthan government has also launched a health insurance scheme to provide medical coverage of up to Rs 3 lakh to each citizen and is expected to cover nearly 70% of the state’s population.
Health insurance is an area where PPP arrangements have been successful. The Yeshasvini Cooperative Farmer’s Healthcare Scheme, a PPP scheme involving Narayana Health and the Karnataka government, offers coverage of over 800 surgical procedures to farmers and their family members. Yeshasvini is one of the largest self-funded healthcare insurance schemes in the country. Neighbouring Andhra Pradesh runs the Arogya Raksha Scheme in collaboration with the New India Assurance Company and with private clinics. The scheme, which is fully funded by the government, provides hospitalisation benefits and personal accident benefits to citizens below the poverty line.
The new Companies Act of 2013 mandates corporates to spend 2% of their profits on CSR activities. The government can take this opportunity to partner with the private sector, leading to a huge improvement in healthcare delivery in India through a combination of good infrastructure, latest technology and the best available medical expertise.

पानी पर केंद्र के हक में ही राष्ट्रहित
देश के 256 जिलों के 33 करोड़ से अधिक सूखे से पीड़ित लोगों के कल्याण हेतु सरकार की चेतना को जागृत करने के लिए प्रबुद्ध समाजसेवियों द्वारा देशव्यापी जल सत्याग्रह का आज समापन है। नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने पानी को लेकर आपातकाल लगाने की बात करके जल संकट पर एक नई संवैधानिक बहस छेड़ दी है। संसद में जब महत्वपूर्ण विषयों पर राजनीतिक गतिरोध चल रहा है तब पानी के बारे में अधिकतर नेताओं का आम-मत होना सुखद है। इसकी बानगी लोकसभा की जल संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में मिलती है, जिसमें पानी को संविधान की समवर्ती सूची में डालने की सिफारिश की गई है। संविधान के अनुच्छेद-262 और केंद्र सूची की प्रविष्टि-56 में दिए गए अधिकार के बावजूद पानी और नदी पर केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है। समवर्ती सूची का कानून अगर पारित हो गया तो पानी के बारे में केंद्र सरकार भी कानून बना सकेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता 30 वर्ष पहले 1986 में ही समझते हुए भू-जल पर केंद्र सरकार के अधिकार पर जोर दिया था। संसद की लोक लेखा समिति की 2014-15 की आठवीं रिपोर्ट में जल-प्रदूषण की चर्चा करते हुए पानी को समवर्ती सूची में लाने की बात की गई है। भाजपा तथा टीआरएस के कुछ सांसदों ने पानी को समवर्ती सूची में लाने के लिए प्राइवेट बिल भी पेश किए हैं। शिक्षा, बिजली एवं चिकित्सा जैसे विषय संविधान की समवर्ती सूची में हैं। उसी तर्ज पर पानी भी संविधान की समवर्ती सूची में आने से जल संकट से निपटने में आसानी होगी। आलोचकों के अनुसार पानी को केंद्र सरकार के दायरे में लाने से निजीकरण तथा बाजारवाद हावी होने की उम्मीद है, पर ऐसे खतरे तो पानी पर राज्य सरकार के नियंत्रण में ज्यादा हैं।
बढ़ती आबादी के साथ नदियां सिकुड़ रही हैं और भूजल स्तर खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा है। देश में पानी के 6,607 ब्लॉक्स हैं, जिनमें 2,000 ब्लॉक्स में पानी के अत्यधिक शोषण से हालत गंभीर हो गई है। बढ़ती आबादी और उपभोग से आजादी के 70 साल बाद देश में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता एक-चौथाई ही रह गई है। पिछले साल देश में लगभग 1879 अरब घन मीटर सालाना पानी उपलब्ध था, जिसमें सिर्फ 1123 अरब घन मीटर का ही इस्तेमाल हो पाया था। बकाया पानी के बेहतर प्रबंधन एवं इस्तेमाल के लिए देशव्यापी नज़रिये की जरूरत है, क्योंकि पानी राज्यों की सीमाओं के राजनीतिक भूगोल को नहीं समझता। प्रगतिशील राज्यों ने इस बात को पहले ही समझ लिया था, जिस वजह से डैम सुरक्षा विधेयक 2010 हेतु बंगाल और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकार को पानी के बारे में कानून बनाने का अधिकार दे दिया था। सूखे पर केंद्र सरकार की मदद मांगने वाले राज्य पानी को समवर्ती सूची में लाने का विरोध कैसे कर सकते हैं? अभी हाल में 10 राज्यों ने सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 42,143 करोड़ रुपए की मांग की है। लातूर में पानी के संकट पर केंद्र सरकार तथा रेल मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन से पानी भेजा गया। पंजाब द्वारा सतलज जल संधि के उल्लंघन पर हरियाणा ने केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख अधिकारों के संरक्षण की गुहार लगाई थी, जिससे पानी पर केंद्र सरकार के अधिकार का तर्क संगत मामला बनता है।
सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख 2002 में एक रोचक मामला आया, जिसमें नदियों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हुए उन्हें आपस में जोड़ने की बात थी। नदियों को जोड़ने की योजना कांग्रेस के शासन काल में केएल राव ने 1972 में बनाई थी। इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मूर्तरूप देते हुए टास्कफोर्स का गठन किया, जिसके मुखिया सुरेश प्रभु बनाए गए थे। जनहित याचिका में दस साल की लंबी सुनवाई के बावजूद 2012 के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने नदियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं पारित किया। क्रियान्वयन में विलंब से प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़कर 11 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गई है और अब इसका क्रियान्वयन इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राज्य पानी की अधिकता को मानने के लिए तैयार नहीं है। पर्यावरण, विस्थापन एवं अन्य कारणों से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आशंका व्यक्त की जा रही है। विरोध के आधार पर प्रोजेक्ट रोकने की बजाय समस्याओं का निराकरण होना आवश्यक है। योजना में विलंब से बुंदेलखंड, विदर्भ, कालाहांडी और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में भयानक मानवीय त्रासदियां पैदा हो रही हैं, जिस वजह से देश में पानी का आपातकाल लागू करने की बात होने लगी है। अर्थव्यवस्था के फैलाव में जैसे खनिज पदार्थों का ट्रांसफर होता है वैसे ही मानवीय समाज को बचाने के लिए पानी का नदियों से ट्रांसफर हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि मजबूरी भी है।
विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत जैसे जल संकट वाले देशों को 2050 तक जीडीपी में 6 फीसदी तक की हानि हो सकती है। भारत में विश्व की 18 फीसदी आबादी है पर पानी के स्रोत सिर्फ 4 फीसदी हैं। अगर हम बढ़ती आबादी पर नियंत्रण पर असफल रहे हैं तो पानी के प्रबंधन के नए तरीके अपनाने ही होंगे। एनसीएईआर की रिपोर्ट के अनुसार पानी के बेहतर प्रबंधन से खाद्य पदार्थों के उत्पादन में दो फीसदी वृद्धि होने के साथ सिंचाई में 33 एमएच की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे 34,000 मेगावाट जल-विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन होने के साथ रोजगार में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना है इससे ग्रामीण समाज में एक नई कृषि क्रांति हो सकती है।
सूखती नदियों की बड़ी जवाबदेही राजनेताओं की है, जो राज्यों में संगठित तौर पर अवैध माइनिंग करवाते हैं। सूखाग्रस्त इलाकों में पानी के कारोबार से भी राजनेता संपन्न हो रहे हैं। राज्यों के बीच पानी की लड़ाई से किसानों की फसल को फायदा हो या न हो पर दलों की चुनावी फसल जरूर अच्छी हो जाती है। पानी राष्ट्रीय संपत्ति है, जिसके बेहतर उपयोग के लिए केंद्रीय नियमन होना ही चाहिए। संसद में कई महत्वपूर्ण विषयों पर गतिरोध है पर पानी को समवर्ती सूची में लाने के बारे में संविधान संशोधन कानून को सभी दलों का समर्थन मिलेगा, यह उम्मीद तो प्यासा देश कर ही सकता है? पूर्ववर्ती यूपीए सरकार तथा वर्तमान एनडीए सरकार ने पानी को समवर्ती सूची में लाने की पैरवी की है। राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर पानी के कानून को पारित करके क्या राजनेता देश को जोड़ पाएंगे? पानी के आपातकाल के इस भयानक दौर में सामूहिक विमर्श और सहमति ही देश के पानी और खुशहाली को बचा पाएंगे।