
03-05-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:03-05-23
Date:03-05-23
JCBs Not The Answer
Unauthorised colonies are an Indian urban reality. Demolishing them is both cruel and economically irrational.
TOI Editorials
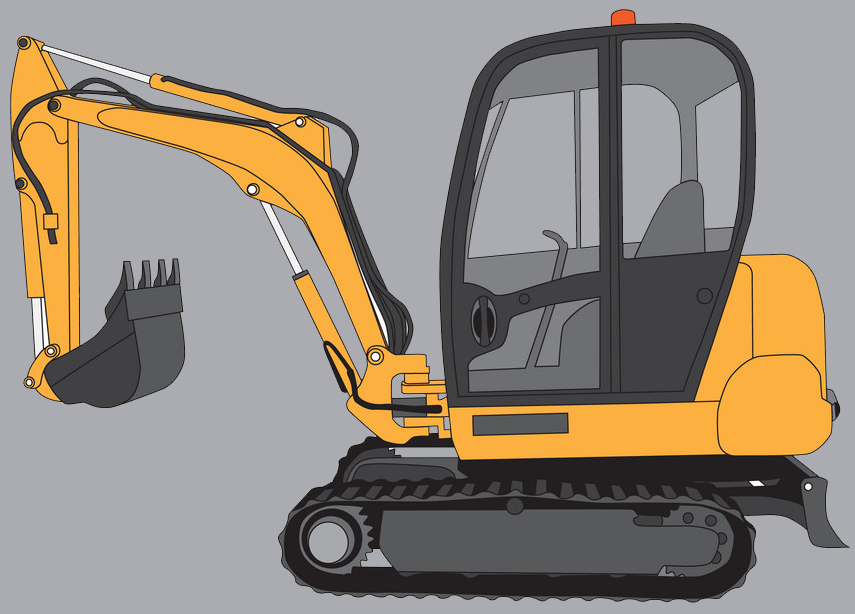
India’s first-ever urban master plan was designed for Delhi in 1962. It was followed by six decades of failure as none of the master plans checked the proliferation of the “silent sprawl”. Unrealistic master plans in Delhi, and other big cities, were overwhelmed by the emergence of cities as India’s main engine of economic growth. Today, the Delhi Development Authority estimates that at least 5 million live in unauthorised colonies spread over 175 sq km. Inhabitants of these colonies are integral to the capital’s economic and social life.
Without them, the city will hollow out.
Successive governments in Delhi have recognised this and tried to regularise these colonies. In December 2019, GoI enacted a law to recognise the property rights of residents of unauthorised colonies. Property titling not just safeguards a lifetime’s savings, it also opens the door to greater access to the formal financial system. This has been the underlying motive of other state governments that have worked out schemes to regularise properties in urban growth engines such as Mumbai and Bengaluru. It shouldn’t be forgotten that in some cases civic authorities have even levied and collected property tax prior to regularisation. It shows that unauthorised colonies are not black spots. They show up in the documents of different arms of the state. Yet, as it happened in Tughlaqabad, they remain highly vulnerable to clearance drives.
Despite laws to protect them, outcomes have been unsatisfactory, reducing opportunities for millions of urban dwellers. It’s unfair they have to pay the price for failures in urban planning and corruptionin the executive. Also, solutions have to be realistic. Relocating people miles from their workplace is cruel when Indian cities have a poor public transport system. Unauthorised colonies are our urban reality. Fast-tracking property titles is the only way out.
A good divorce
Irretrievable breakdown of marriage should be a ground for divorce.
Editorial
Not all marriages are happy, and not all divorces are unhappy. For those who want to opt out of a bad marriage, Monday’s Supreme Court ruling on divorce will be seen as a good move. Leaning on the “guiding spirit” of Article 142(1) of the Constitution to do “complete justice” in any “cause or matter”, a Constitution Bench said it could use this extraordinary discretionary power to grant divorce by mutual consent to couples trapped in bitter marriages. It also aims to spare couples the “agony and misery” of waiting six to 18 months for a local court to annul it, as stipulated under Section 13B of the Hindu Marriage Act, 1955. The Bench, headed by Justice Sanjay Kishan Kaul, observed that the law of divorce, built predominantly on assigning fault, fails to serve broken marriages. It pointed out that if a marriage is wrecked beyond hope, public interest lies in recognising this fact, not upholding a ‘married’ status regardless. The Court said it could use Article 142 to quash pending criminal or legal proceedings, be it over domestic violence or dowry, against the man or woman. Continuing in this strain, the Bench said the Supreme Court could grant divorce on the grounds of an “irretrievable breakdown of marriage” if the “separation is inevitable and the damage is irreparable”. Under the Hindu Marriage Act, irretrievable breakdown of marriage is not yet a ground for divorce.
In its judgment, there was a word of caution that the grant of divorce would not be a “matter of right, but a discretion which is to be exercised with great care… keeping in mind that ‘complete justice’ is done to both parties.” Several factors would be considered by the Supreme Court before invoking Article 142 in matrimonial cases, including duration of marriage, period of litigation, the time the couple has stayed apart, the nature of pending cases, and attempts at reconciliation. The Court will have to be satisfied that the mutual agreement to divorce was not under coercion. In India, while divorcees have doubled in number over the past two decades, the incidence of divorce is still at 1.1%, with those in urban areas making up the largest proportion. But the divorce numbers do not tell the whole story; there are many women, particularly among the poor, who are abandoned or deserted. Census 2011 revealed that the population which is “separated” is almost triple the divorced number. In a country which is largely poor, where gender discrimination is rife and many women are still not financially independent, the Court’s stress on “care and caution” and not to rush into a quick divorce must be welcomed. After all, marriage equality is not a reality for all.
मजबूत लोकतंत्र की पहली शर्त – स्वतंत्र प्रेस
संपादकीय
एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चार मूल तत्वों का होना जरूरी है- बहुमत का शासन, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मान्यता, संवैधानिक सरकार और सबसे महत्वपूर्ण संवाद के जरिए शासन कोई चुनी हुई सरकार यह कहकर शासन नहीं चला सकती कि वह जनता के वोटों से एक निश्चित समय के लिए चुनी गई है। लिहाजा उस काल-खंड के बाद ही जनता को जवाब देगी। सरकारें जनहित में काम करें, यह उनका मूल दायित्व है न कि कोई अहसान । इसके बरअक्स प्रेस की असली भूमिका लोक-कल्याण के मुद्दों को जन-धरातल तक पहुंचना, मुद्दों के हर पहलू से लोगों को वाकिफ कराना और लोगों की व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना को बेहतर करने के लिए तर्क – शक्ति को समृद्ध करना होता है। कई बार सरकारें ऐसी भूमिका को नकारात्मक मानते हुए प्रेस फ्रीडम को अपने खिलाफ मानने लगती हैं, लेकिन उनका सोचना गलत है। दरअसल, प्रेस की मदद से जनता किसी सरकार के कार्यों का सही आकलन करे, यह जनता के लिए ही नहीं, सरकार के भी दीर्घकालिक हित में होता है। यही कारण है कि अमरीकी संविधान निर्माताओं ने सन् 1789 में संविधान को अंगीकार करने के दो साल बाद ही पहला संशोधन करके अभिव्यक्ति की आजादी के साथ ‘प्रेस फ्रीडम’ को हमेशा संसदीय शक्तियों से परे करार दिया। भारत के संविधान निर्माताओं ने इससे भी व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए अनुच्छेद 19 (1) (अ) में इसे ‘हर नागरिक की अभिव्यक्ति की ‘आजादी’ के रूप में मौलिक अधिकार बनाया। यह अलग बात है कि संविधान अंगीकार करने के डेढ़ साल में ही पहला संशोधन करके अनुच्छेद 19 (2) में तीन और नए प्रतिबंध- लोक-व्यवस्था, मित्र देशों से संबंध और किसी अपराध के लिए उकसाना जोड़ दिए गए। भारत में भले ही अभिव्यक्ति की आजादी सभी नागरिकों के लिए हो, लेकिन व्यवहार में औपचारिक प्रेस को यह स्वतंत्रता न केवल देना बल्कि उसे मजबूत करना प्रजातंत्र की पहली शर्त है।
Date:03-05-23
प्रेस आजाद है लेकिन अंकुश लगाने की कोशिशें भी जारी
पवन के. वर्मा, ( लेखक, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद )
हर साल 3 मई को यूएन और यूनेस्को द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हमारी तमाम स्वतंत्रताएं कमोबेश मीडिया की आजादी से जुड़ी हैं। भारत में संविधान के 19वें अनुच्छेद ने अभिव्यक्ति की आजादी को बुनियादी अधिकारी निर्दिष्ट किया है, जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता भी निहित है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस की 30वीं वर्षगांठ एक अवसर है कि हम देश में मीडिया की आजादी का संतुलित विश्लेषण करें।
एक बात तो साफ है, भारत के लोग बीते सात दशकों में लोकतंत्र के अभ्यस्त हो चुके हैं और वे प्रेस की आजादी को महत्व देते हैं। वे सरकारी प्रोपगंडा और तटस्थ समाचार के बीच के भेद को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। यह कोई आज की बात नहीं है। 1975-77 में आपातकाल के दौरान जब सरकार के नियंत्रण वाला दूरदर्शन उसके गुण गाता था, तब भी ग्रामीण क्षेत्रों तक के लोग वास्तविकता जानने के लिए बीबीसी रेडियो लगा लिया करते थे। सरकारें चाहे जिस विचारधारा की हों, वे ऐसे ‘सहयोगी’ मीडिया को महत्व देती हैं, जो उनकी प्राथमिकताओं को सामने रखे, नीतियों का प्रचार करे और उनकी कम से कम आलोचना करे। चूंकि मैं भारत के दो राष्ट्रपतियों के प्रेस सेक्रेटरी की भूमिका निभा चुका हूं और विदेश मंत्रालय के अधिकृत प्रवक्ता के रूप में भी सेवाएं दे चुका हूं, इसलिए मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। सरकार अनेक तरीकों से लक्ष्यों को अर्जित कर सकती है : वे मीडिया बना सकती हैं, विचारकों को प्रभावित कर सकती हैं, मीडिया आउटलेट्स पर स्वामित्व रखने वाले कॉर्पोरेट्स से मैत्री बना सकती हैं इत्यादि। लेकिन मीडिया प्लेटफॉर्मों को धमकाने, उन पर दबाव बनाने, उन्हें दंडित करने- जिसमें उन्हें विज्ञापन नहीं देना भी शामिल है- लोकतंत्र की सीमारेखा को लांघने वाली गतिविधि कहलाएगी।
क्या सरकार ने यह सीमारेखा लांघी है? हां और ना दोनों। यह तो कोई भी नहीं कह सकता कि भारत में स्वतंत्र मीडिया नहीं है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि उस पर अंकुश लगाने की कोशिशें नहीं हुई हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत 2022 में दुनिया के 180 देशों में 150वें स्थान पर था। यह अब तक की सबसे निचली रैंकिंग थी। उसकी पोजिशन 2017 के बाद से ही निरंतर गिरती रही है। यह इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ बनाता है। वे अपनी रैंकिंग के लिए अनेक महत्वपूर्ण सूचकांकों का उपयोग करते हैं। इनमें मीडया की स्वायत्तता, उस पर राजनीतिक दबाव, नेताओं और सरकार को जवाबदेह ठहराने की आजादी, पत्रकारों की निजी और पेशेवर सुरक्षा आदि शामिल हैं।
सरकार ने इस रिपोर्ट से असहमति जताई है। लेकिन हाल के समय में कुछ परेशान कर देने वाले ट्रेंड्स उभरे हैं, जिनकी अनेदखी नहीं की जा सकती। पहला यह है कि सरकार की किसी भी तरह की आलोचना को राष्ट्रविरोधी या राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध करार दे दिया जाता है। संविधान ने अनुच्छेद 19(2) में राज्यसत्ता को अधिकार दिए हैं कि वह भारत की सम्प्रभुता व एकता की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने, अदालत की अवमानना या लोगों को उकसाने वाली किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी पर ‘समुचित प्रतिबंध’ लगा सकती है। लेकिन वर्ष 2020 में जब एक मलयाली चैनल मीडिया वन टीवी को सरकार द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था तो सर्वोच्च अदालत ने इस आदेश को उलटते हुए स्पष्ट कहा था कि सरकारी नीतियों की आलोचना को अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। वर्ष 2021 में जब दिवंगत पत्रकार विनोद दुआ पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था तो सर्वोच्च अदालत ने एफआईआर को खारिज करते हुए मीडिया पर मनमानी कार्रवाई की प्रवृत्ति को आड़े हाथों लिया था। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि प्रेस की जिम्मेदारी है सत्ता को सच बताना और सरकार इसे नीतियों की आलोचना करार देते हुए उस पर अंकुश नहीं लगा सकती। 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च अदालत ने आईटी एक्ट के अनुच्छेद 66(ए) को भी समाप्त कर दिया था, क्योंकि यह ‘आपत्तिजनक’ समझी जाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट्स के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने की अनियंत्रित शक्तियां पुलिस को देता था।
तलाक की अवधि
संपादकीय
भारतीय समाज में विवाह एक सामाजिक परंपरा है, लेकिन यह इस संबंध में बने कानून के दायरे में भी है। अगर किन्हीं कारणों से पति और पत्नी के बीच दरार आ जाती है और सुलह नहीं हो पाती तथा संबंध आखिर अलगाव के रास्ते की ओर बढ़ जाता है, तो इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया रही है। उसमें अंतिम फैसले तक पहुंचने से पहले खास अंतराल भी तय किया गया है। मगर इस मसले पर जिस तरह की नई परिस्थितियां बन रही हैं और जैसी जटिलताएं उभर रही हैं, उसके मुताबिक इस संबंध में नई व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की एक पांच सदस्यीय पीठ ने अब विवाह विच्छेद या तलाक को लेकर यह व्यवस्था दी है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के मुताबिक आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए निर्धारित छह से आठ महीने की प्रतीक्षा अवधि को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकती है। जाहिर है, अब अगर पति और पत्नी के आपसी रिश्तों में किसी भी वजह से आ गई दरार को खत्म कर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो उसके हल के रूप में तलाक लेने के लिए पहले की तरह कम से कम छह महीने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं रह जाएगी।
शीर्ष अदालत ने इस बिंदु पर कहा कि पति-पत्नी के बीच आई दरार को पाटना संभव नहीं हो पा रहा है तो ऐसी शादी को आपसी सहमति के आधार पर छह महीने से पहले भी खत्म किया जा सकता है। दरअसल, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के मुताबिक अभी तक जो व्यवस्था रही है, उसमें आपसी सहमति से तलाक की मांग करने वाला प्रस्ताव दाखिल करने के बाद पक्षकारों को दूसरा प्रस्ताव पेश करने से पहले कम से कम छह महीने और अधिकतम अठारह महीने तक इंतजार करना पड़ता था। इसका उद्देश्य यह था कि तलाक के लिए अर्जी देने वाले दोनों पक्षों को अपने फैसले पर आत्मनिरीक्षण करने के निर्णय पर फिर से विचार करने का अवसर मिल सके। ऐसे मामले भी हैं, जिनमें आपसी विवाद तात्कालिक तौर पर तो अलगाव की स्थिति पैदा करता है, लेकिन थोड़ा वक्त बीतने के साथ दोनों पक्षों के भीतर थोड़ी नरमी आती है और कभी अलग होने का फैसला बदल भी सकता है। ऐसी स्थिति में कानूनन पति और पत्नी के नए रुख के आधार पर ही अदालत का फैसला आता है।
कई मामलों में तलाक का प्रस्ताव अदालत में पेश किए जाने के बाद कानूनी तौर पर निर्धारित प्रतीक्षा की अवधि कठिनाई बनती देखी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद इस मसले की जटिलता थोड़ी आसान हुई है। यह छिपा नहीं है कि वक्त के साथ लोगों के सोचने-समझने और खुद को बरतने का तौर-तरीका बदला है। खासकर अगर पति और पत्नी के बीच किन्हीं वजहों से ऐसी दरार आ गई हो, जिसके हल की कोई भी गुंजाइश न बची हो तो ऐसे में साल-डेढ़ साल की अवधि इंतजार करना बेमानी लगता है। कभी-कभी एक पक्ष तलाक को अंतिम हल मानता है, मगर दूसरा पक्ष इसका विरोध करता है। ऐसी स्थिति में शीर्ष अदालत का ताजा फैसला नई दिशा देगा। किसी भी सामाजिक बदलाव और इसके लिए लोगों को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है और उसका हल कई बार कानून के जरिए निकालना आसान होता है।
Date:03-05-23
सामाजिक सुरक्षा से टिकाऊ विकास
अरविंद कुमार मिश्रा
वैश्वीकरण के साथ सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न अब किसी एक देश का मुद्दा नहीं रह गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सत्रह सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य शर्त है। सामाजिक सुरक्षा का स्तर गरीबी, असमानता, जातिगत और जेंडर भेद को समाप्त करने का सबसे अहम जरिया है। इसके जरिए औपचारिक क्षेत्र को संगठित कार्यबल में तब्दील किया जा सकता है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 के वार्षिक सम्मेलन में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा चर्चा में है। इसके कार्यसमूह में श्रम-20 द्वारा पांच बड़े मुद्दों को उठाया गया है। पहला, श्रमिकों का प्रवासन, दूसरा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, तीसरा, कौशल प्रशिक्षण और कौशल उन्ययन (नियोक्ता की भूमिका और दायित्व), चौथा, कार्य का बदलता स्वरूप और पांचवां, टिकाऊ तथा सम्मानजनक आजीविकाओं को प्रोत्साहन।
ये पांचों मुद्दे सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हैं। इसकी जरूरत को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) द्वारा जारी विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 के तथ्यों से समझा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व में तिरपन फीसद आबादी सामाजिक सुरक्षा से वंचित है। छियालीस प्रतिशत लोग ही रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन जैसी किसी एक सामाजिक सुरक्षा का लाभ हासिल कर पा रहे हैं। 18.6 प्रतिशत बेरोजागर युवकों को मुश्किल से बेरोजगारी भत्ता मिल पाता है। 26.4 प्रतिशत बच्चों को ही सामाजिक सुरक्षा की चादर नसीब है। गंभीर दिव्यांगता के शिकार सिर्फ 33.4 प्रतिशत लोग समाज की मुख्यधारा में शामिल हैं। आज भी छियालीस फीसद महिलाएं मातृत्व अवकाश से वंचित हैं। तैंतीस फीसद आबादी को स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया जाना है। बाईस फीसद बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन न मिलने से जीवन के अंतिम पड़ाव पर चुनौतियों से जूझते हैं।
दुनिया भर का पचासी फीसद कारोबार जी-20 देशों के बीच होता है, जबकि पैंसठ फीसद आबादी यहां रहती है। विश्व के कुल कार्यबल का इकसठ प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में आता है। अफ्रीका में 85.8 फीसद रोजगार असंगठित क्षेत्र में हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 68.6 और 68.6 फीसद अरब देशों में तथा अमेरिका में चालीस प्रतिशत और यूरोप में यह अनुपात 25.1 फीसद है। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के स्तर को प्रभावी बनाकर असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में रूपांतरित करने में मदद मिलेगी। आइएलओ ने 1952 में हुए सम्मेलन के दौरान सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम नौ आधार बताए थे। इनमें स्वास्थ्य देखभाल, बीमारियों में बीमा लाभ, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, कार्यस्थल पर मुआवजा, पारिवारिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ, अशक्तता और उत्तरजीविता लाभ शामिल हैं।
2016 में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने संयुक्त रूप से सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पर काम करने का आह्वान किया। अगर जी-20 देशों के बीच सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पर ठोस सहमति बनती है, तो प्रवासन से जुड़ी चुनौतियां का समाधान होगा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही प्रवासन की चुनौतियां अलग हैं। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों को भविष्य निधि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इन प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ देने के लिए तीन व्यवस्थाएं हो सकती हैं। दो देशों के बीच द्विपक्षीय करार हो, ब्रिक्स, बिम्सटेक और अफ्रीकी संघ इसे लागू करें, ठीक वैसे ही जैसे यूरोपीय यूनियन ने किया है। मगर यदि इसे वैश्विक आवरण देना है, तो जी-20 देशों के बीच बहुपक्षीय समझौता ठोस विकल्प होगा।
सामाजिक सुरक्षा की कोई भी कार्ययोजना श्रमिक, नियोक्ता, सरकार और श्रम संगठनों के एकजुट प्रयासों से ही संभव है। दुनिया भर में श्रमिक संगठन अपनी विचारधारा के आधार पर श्रम सुधार और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। भारत में जी-20 के अंतर्गत आयोजित श्रम-20 में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनों ने जिस प्रकार एकजुटता दिखाई, वह अच्छा संकेत है। जी-20 के पिछले कुछ सम्मेलन श्रम जगत को लेकर प्रतिबद्धताएं जाहिर करने तक ही सीमित रहे हैं। 2020 में रोम घोषणा-पत्र में डिजिटल संसाधनों से श्रम क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा को गति देने का आह्वान किया गया, वहीं 2022 का बाली घोषणा-पत्र सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित लच्छेदार भाषणों तक सीमित रहा। 2015 में तुर्किए जी-20 सम्मेलन के दौरान ‘अंटाल्या यूथ गोल’ पर सहमति बनी। इसके अंतर्गत 2025 तक बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं के अनुपात में पंद्रह फीसद कटौती की जानी थी। हालांकि उस सम्मेलन के आठ साल बीत जाने के बाद जी-20 के वार्षिक सम्मेलनों में यह मुद्दा सिर्फ घोषणा-पत्र में उल्लेख किए जाने तक सीमित है।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च बढ़ाकर ही सतत विकास लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। सबसे पहले इन योजनाओं को वित्त पोषण और संसाधन जुटाने के लिए घरेलू स्तर पर टिकाऊ वित्त की व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। भारत में सामाजिक सुरक्षा पर जीडीपी का लगभग 1.4 प्रतिशत व्यय होता है। इंडोनेशिया में यह 1.3 फीसद, दक्षिण अफ्रीका में 5.5, चीन में 7.7, ब्रिटेन में 15.1 और अमेरिका में 18.9 प्रतिशत है। इसमें सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा व्यय में वैयक्तिक और परिवारों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं और स्थानांतरण पर खर्च और सामूहिक सेवाओं पर व्यय शामिल है। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के लिए आवश्यक टिकाऊ वित्त व्यवस्था करने की अहम जिम्मेदारी जी-20 में शामिल जी-7 (अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन) की भी है। इन देशों के पास दुनिया के सत्तासी फीसद आर्थिक संसाधन हैं।
भारत के लिए जी-20 का वर्तमान आयोजन वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने का बड़ा मौका है। इससे आखिरकार वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच आर्थिक असमानता की खाई कम होगी। अमेरिका में 64.3 फीसद, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 44, अरब देशों में 40, जबकि अफ्रीकी देशों में सिर्फ 17.4 प्रतिशत लोगों को कोई एक सामाजिक सुरक्षा हासिल है। इथियोपिया के आदिस अबाबा में जी-20 सम्मेलन के दौरान सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ‘इंटिग्रेटेड नेशनल फाइनेंस फ्रेमवर्क’ अस्तित्व में आया था। इसे व्यावहारिक रूप से अब तक लागू नहीं किया जा सका है। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा ऐसी हो, जो आर्थिक रूप से हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो, वहीं यह वहनीय हो। इससे क्षेत्रीय असमानता भी दूर होगी। आर्थिक महाशक्तियों में भी सामाजिक सुरक्षा का दायरा बहुत बेहतर नहीं है। यूरोप और मध्य एशिया में सामाजिक सशक्तिकरण पर आधारित योजनाएं सरकार प्रायोजित पहल में सिमटी हैं।
भारत में जनधन, आधार और मोबाइल (जेएएम) के जरिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को नई ऊंचाई दी जा रही है। आधार के जरिए 318 केंद्रीय योजनाओं और राज्यों की 720 योजनाएं संबद्ध हैं। यह नकद हस्तांतरण योजना को सफल बनाने में सबसे कारगर जरिया बनी है। 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 135.2 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। इनमें 75.3 करोड़ नागरिकों तक राशन मुहैया कराने और 27.9 करोड़ उपभोक्ताओं तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने में आधार पहचान-पत्र के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तरह 75.4 करोड़ बैंक खाते आधार से जोड़े जा चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का बड़ा जरिया बनी है। इसके शहरी संस्करण पर भी विचार होना चाहिए। भारत में अस्सी फीसद लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। आइएलओ के मुताबिक देश की 24.4 प्रतिशत आबादी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में है। समग्र रूप से कहें तो सामाजिक संरक्षण पर जितना अधिक खर्च होगा, गरीबी का स्तर उतना ही निम्न होता चला जाएगा।
अलगाव में सहूलियत
संपादकीय

ताकि तलाक अभिशाप नहीं, नए जीवन का मोड़ बन जाए
कमलेश जैन, ( वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट )
पहली मई को सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ ने शिल्पा शैलेश और वरुण श्रीनिवासन के मुकदमे में पति-पत्नी के बीच वर्षों से चली आ रही उलझनों का स्थायी निवारण कर दिया। इसके साथ तीन अन्य दंपतियों (नीति मालवीय बनाम राकेश मालवीय, अंजना किशोर बनाम पुनीत किशोर, और मनीष गोयल बनाम रोहिणी गोयल) के मुकदमों का भी फैसला सुनाया गया। कुल 61 पृष्ठों में आए इस निर्णय से तलाक आसान बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाए गए हैं। दरअसल, वैवाहिक मामलों में दरार पिछले दो-ढाई दशकों में बढ़ी है। इस दरम्यान संसद से नए-नए कानून बने, जिनकी वजह से रिश्तों में सुधार होने के बजाय उलझन बढ़ती गई और अदालतों पर तलाक के मुकदमों को बोझ बढ़ता गया। इसकी शुरुआत 1983 से हुई है, जब 25 दिसंबर को भारतीय दंड संहिता में धारा 498-ए जोड़ा गया। इसने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने या अन्य प्रकार की क्रूरता करने के लिए पति और उसके परिजनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना आसान बना दिया। इसके तहत एफआईआर दर्ज होते ही पूरा परिवार, चाहे वह अलग-अलग राज्यों में रहता हो, गिरफ्तार कर लिया जाता, बेशक मुकदमे की विवेचना बाद में होती।
इस बाबत एक जनहित याचिका (रिट पिटिशन नंबर 8/2003) मैंने खुद सर्वोच्च न्यायालय में 2003 में डाली थी, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि वह ऐसा करने में असमर्थ है। उसने इसके लिए संसद और भारतीय विधि आयोग को आदेश व याचिका की कॉपी भेजने की बात कही थी। बाद के वर्षों में बदलाव हुआ, और अब परिवार जेल नहीं जाता, सिर्फ पति जा सकता है, वह भी स्पष्ट आधार पर। घरेलू हिंसा कानून का भी इसी तरह बेजा लाभ उठाया जाता रहा, जबकि इसमें आप सभी समस्याओं को एक ही अदालत में रख सकते हैं, जैसे तलाक, भरण-पोषण का खर्च, अलग घर या उसी घर में ठीक से रहने की व्यवस्था, बच्चों का समाधान, क्रूरता (मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, यौनिक आदि) से छुटकारा आदि। इसमें पति या किसी रिश्तेदार को जेल भेजे बिना सभी समस्याओं का समाधान संभव है। मगर कुछ स्त्रियों को यह रास्ता पसंद नहीं। ऐसे मामलों में अक्सर लड़का ही झुकता है, ताकि उसका परिवार शांति से रह सके। इसके लिए वह बतौर मुआवजा बड़ी राशि देने को भी तैयार हो जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय का ताजा फैसला इन तमाम मुश्किलों का समाधान कर सकता है। यह फैसला इस आधार पर किया गया है कि जिस रिश्ते में ऐसी खाई बन गई है, जिसको पाटा न जा सके, उसमें तलाक के लिए छह महीने का इंतजार आखिर क्यों किया जाए? अगर पति-पत्नी में वर्षों का अलगाव है, तो उसका यही अर्थ है कि उनमें जुड़ने की इच्छा मर चुकी है। इसका मकसद यह भी है कि युवावस्था में जुड़े जोड़े अनंतकाल तक अदालतों में दौड़ते-दौड़ते बूढ़े न हो जाएं, बल्कि वे समय से नए जीवन की शुरुआत कर सकें। आज स्थिति यह है कि निचली अदालतों से लेकर, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों तक तलाक के मुकदमों की भरमार है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ उत्तर प्रदेश के परिवार न्यायालय में 61,000 से अधिक मुकदमे लंबित थे। भले ही, अपने देश में तलाक की दर दुनिया में सबसे कम 1.1 प्रतिशत है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 20 वर्षों में तलाकशुदा लोगों की संख्या दोगुनी हुई है, जिसका अर्थ है कि भारत में रिश्तों के टूटने की दर बढ़ने लगी है।
जब पति-पत्नी में संबंध विच्छेद ही एकमात्र रास्ता हो, तो यह प्रक्रिया जितनी सरल हो, उतना अच्छा। इसके लिए संसद को आगे आना होगा। जैसे, ‘इरिट्रीवबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज’ का जिक्र कानून में नहीं है, जबकि न्यायालय करीब एक दशक से इस आधार पर तलाक दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इस फैसले के बाद तलाक के मुकदमे कम हो जाएंगे, इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, पर त्वरित न्याय की दिशा में इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह, तलाक, मुआवजा, बच्चों का निर्णय, घरेलू हिंसा का समाधान आदि एक ही फोरम पर हो, तो कहीं अच्छा होगा। उम्मीद है, संसद ऐसे मामलों में पर्याप्त संजीदगी दिखाएगी।
