
02-12-2022 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:02-12-22
Date:02-12-22
Stats Of The Union
Economic gap between regions in India is growing. It will have consequences in other areas.
TOI Editorials
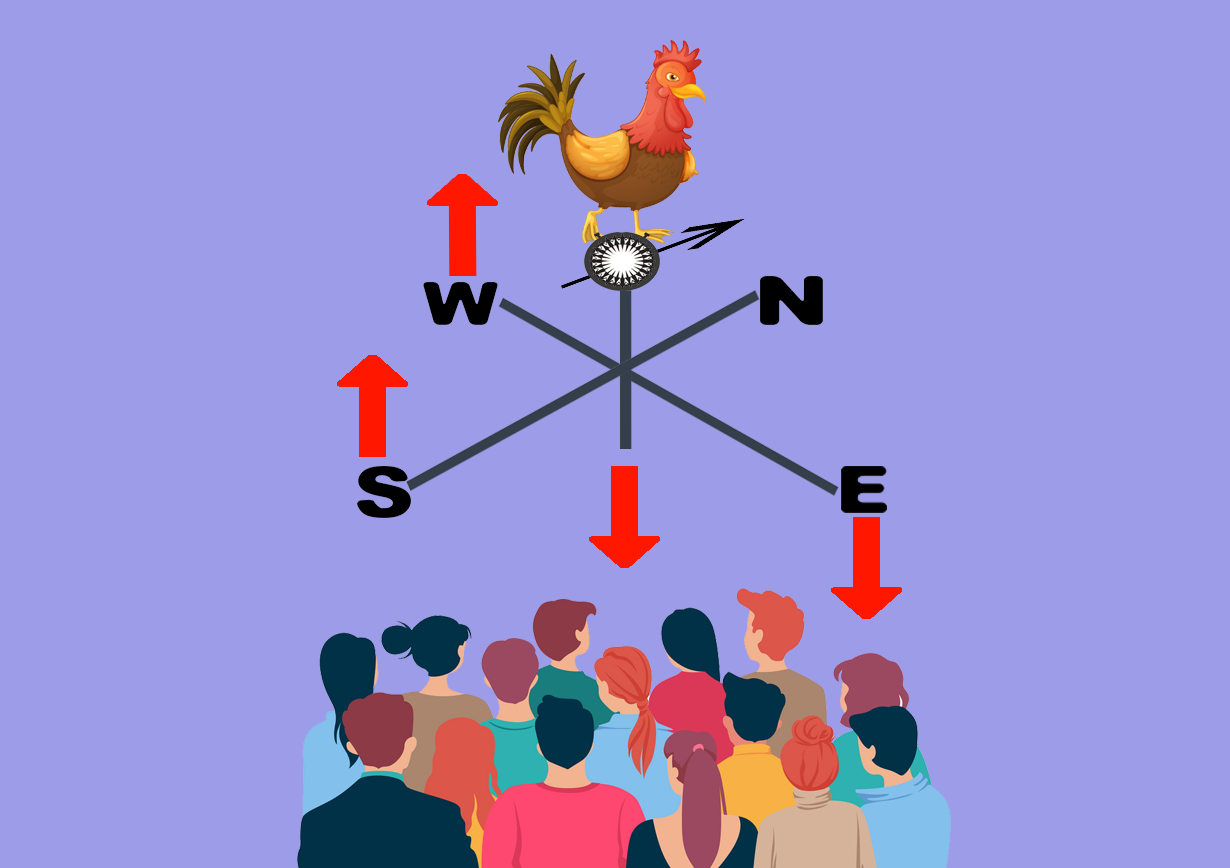
Consider the per capita incomes of Bihar and Karnataka in 1989-90, the eve of economic liberalisation. Karnataka’s per capita income at Rs 2,055 a year was almost two times that of Bihar. In 2019-20, the last pre-pandemic year, the gap had widened to over five times with Bihar’s annual per capita income at Rs 29,794 and that of Karnataka at Rs 1,55,869. This trend generally holds across states, with the west and south of India pulling away from eastern and central Indian states such as UP and MP. A 2016 paper by IDFC Institute observed that India is the only major economy bucking the trend of subnational convergence.
India’s fiscal architecture and related institutions such as finance commission are designed to mitigate the fallout of the gap by allocating the divisible pool of taxes in a manner that brings about a degree of equity between states. However, a combination of economic and fertility divergences makes for an explosive mix. GoI has projected a national population increase of 311 million between 2011 and 2036. Of this increase, only 9% will come from the five southern states, which the Price survey shows currently contribute 30% of national income with 20% of the population.
These trends are playing out in the backdrop of an impending delimitation of political constituencies that can widen fault lines. India’s subnational economic divergence is a trend that deserves more study and policy attention. A lopsided economic structure usually has consequences that ripple out into other areas. Convergence is the only answer to it.
Let the Money Roll Right In
ET Editorials
Migrant workers from India are set to send home a record $100 billion in 2022, despite global headwinds like rising prices, declares the World Bank’s latest Migration and Development Brief (bit.ly/3iuRQS4). This augurs well for the economy. Inward remittances, which account for about 3% of GDP, are a useful source of current account receipts to finance the trade deficit. The estimated 12% rise in remittance flows is helping India retain its spot as the top recipient of remittances. The growth has been attributed to wage hikes and a strong labour market in the US and other OECD countries. The weakening rupee has also supported growth (in rupee terms).
The pandemic saw a dip in remittance flows as Gulf countries like Kuwait and Oman reduced their dependence on expatriate workers. RBI’s fifth survey of remittances for 2020-21 held that the share of Gulf countries declined also due to stricter labour laws and higher work permit renewal fees. The reopening of host economies supported expat employment and their ability to send money home. Significantly, more skilled Indian migrants living in the US, Britain and Singapore are now sending more money home. The average cost of remittances across major money transfer operators, too, has declined due to growing digitalisation.
A caveat: the global economy is volatile, and a slowdown is likely to accentuate the risks of a wider current account deficit. The visible stress in IT companies globally could slow the pace of growth of India’s software export receipts. This means a widening trade deficit may not get bridged by invisibles’ surplus – mainly software exports and inward remittances. India should push for more worker visas with developed economies to help inward remittances grow.
Should there be a panel to appoint Election Commissioners?
Jagdeep S. Chhokar is Co-founder of election watchdog Association for Democratic Reforms and former Professor at IIM, Ahmedabad & S.Y. Quraishi was the 17th Chief Election Commissioner of India.
With a Constitution Bench of the Supreme Court hearing a batch of petitions on having a neutral mechanism for the appointment of members of the Election Commission of India, the debate on having a collegium-like panel to select Election Commissioners has been revived. In a conversation moderated by Abhinay Lakshman, Jagdeep S. Chhokar and S.Y. Quraishi discuss the need for reforming the process of selection. Edited excerpts:
Is there a case for a collegium-like system for the appointment of Election Commissioners (ECs)?
S.Y. Quraishi: Yes, of course. I have been writing this, saying it in the media for a long, long time that there is a case for a collegium, that it would inspire more public confidence. The presence of the Leader of the Opposition in the Lok Sabha (LoP) in the collegium particularly would lend credence to the selection process. Of course, the Chief Justice of India (CJI) is important also. But the LoP politically has a lot more importance and significance if he or she is signatory to the appointment.
Jagdeep S. Chhokar: I agree with what Dr. Quraishi has said about the collegium, whether it is of the Prime Minister, LoP and CJI, or there are also one or two other people. A broader base and consultative system would obviously be [better]. There is no comparison with the current system where the government of the day appoints ECs on its own, with nobody knowing how it is being done. So, any change of that kind will be very, very useful.
The government’s opposition to reform in this area has so far been the limiting jurisdiction of the Supreme Court. And governments over the years have consistently resisted such reform. What do you have to say about that?
S.Y. Quraishi: Yes, we have been writing to the government. Several predecessors and I have written to the government in the last 20-25 years, and the government has been resisting because no government wants to let go of this power, which is why they have not taken any action. When I was appointed as the EC in 2006, I was told by a top functionary in the Prime Minister’s Office that the Prime Minister was of the opinion that the collegium is a good idea and is not avoidable any more, and he thought that perhaps my appointment would be the last under the old system. But it didn’t happen for whatever reason.
As far as the judiciary’s power to look into the issue goes, the judiciary is the guardian of the Constitution, and a free and fair election is [part of] the basic structure of the Constitution. On anything to ensure a free and fair election, the judiciary comes in very much. And in any case, the judiciary is pointing out that Article 324 requires that Parliament will pass an Act about the procedure of appointment and things like that. It has not happened in the last 72 years. So, the Supreme Court is fully justified in pointing this out. In any case, the Supreme Court has not jumped in suo motu. There are PILs before it, and people have gone to court in protest against the government’s inaction. So, the Supreme Court has every right to ask questions and adjudicate. Why has the government been sleeping for 72 years? Why haven’t they passed this?
Jagdeep S. Chhokar: The reason is obvious. The government wants to have complete control on the constitutional body called the Election Commission of India (ECI), which under the Constitution is supposed to be independent of the government. They have not, in a sense, been resisting. A lot of proposals have been made by the ECI and by several committees and commissions appointed by the government itself for the last 25-30 years. There have been Law Commission reports; there is a report of the commission to review the working of the Constitution; and going back before that, there was the Goswami Committee report, and so on. So, the government’s own commissions and committees have said so, but obviously any government, irrespective of the party in power, wants to have some control over the ECI and appointing ECs directly without consulting anybody else is one obvious way of asserting its power. The government wants to make sure that the ECI, or the three members of the ECI do not have the courage to go against the government’s will. That is the whole issue.
Election Commissioners are considered a feeder category for appointment as CEC, with different thresholds for termination of service. What is the power dynamic being created because of this? And is there a case to consider the appointment of ECs and CECs separate from each other?
Jagdeep S. Chhokar: There is no such provision either in the Constitution or in law, which has been made in 1991 called the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991. Section 4 of that unambiguously says the CEC or an EC shall hold office for a term of six years from the date he or she assumes office. Then there is a proviso, provided that where the CEC or an EC attains the age of 65 years before the expiry of the said term of six years, he or she shall vacate the office on the date on which he or she attains the said age. Now, the trick here is that the government, in its wisdom over the years, has been appointing people as ECs who do not even have six years before they complete 65 years of age, and therefore they attain 65 and they retire as an EC, or at best as the CEC after a tenure of one or two years as the CEC. But there is nothing in the law or in the Constitution which says that you cannot appoint a 58- or 59-year-old. Why can’t the government appoint a 58- or a 59-year-old person as the EC and a different 58- or 59-year-old person as the CEC?
The tradition has been built up obviously by the bureaucracy, so everywhere seniority in the bureaucracy is made to count. The position of EC or CEC is not based on one’s standing or seniority in the civil service. It could even be a lawyer, it could be a judge, I mean it is not a written rule anywhere. The argument given is that bureaucrats conduct elections in the districts when they are District Magistrates and so on, and therefore they have experience that nobody else has. While judges and lawyers and other people who deal with such matters could very well be appointed and even bureaucrats could be appointed at the appropriate age, the intention is not to give any EC or CEC confidence that he or she cannot be touched for the next six years. And that is why this so-called tradition, or the system, has been evoked where batch seniority is extremely important. It is very interesting to see that seniority becomes extremely important for ECs, but within the civil service people are superseded every now and then. Then the principle of seniority is not sacrosanct. So, this issue of whether an EC and a CEC should have a fixed tenure of six years is extremely important, and I am very happy that the Constitution Bench in the Supreme Court took note of it on its own. I think that is a matter which is very important and the ECs and CECs must have a tenure of six years which is undisturbed; and to say that an EC is always elevated to the post of CEC, that again is a created situation. The Constitution or the law does not say that anywhere at all. All three members are equal, and one is first among equals.
S.Y. Quraishi: I think the seniority principle is an important principle to follow, even in the Supreme Court. The short tenure of the CEC does not infringe on his or her independence. That is an independent issue. And the short tenure is happening because since 1993, we have a multi-member ECI, and we have to see the combined tenure as EC and CEC, or 65 years of age, whichever is earlier.
Given that the kind of protection from termination is different for ECs and the CEC, does this not significantly complicate the position a CEC might be in after having served as EC for part of his or her tenure?
S.Y. Quraishi: Yes, which is why we say that while the CEC is protected from removal, the two ECs are not, which was a mistake committed at the time of passing the 1993 amendment. It should have been automatic because protection to an EC is not for the individual but for the institution. The institution was a one-member institution earlier, now it is a three-member institution. So, protection has to extend to all three.
युवा भारत अगले 15 वर्षों में क्या चीन को पछाड़ेगा ?
संपादकीय
इस वर्ष से चीन में आबादी का ढलान शुरू हो गया जबकि अगले वर्ष भारत की जनसंख्या 142.863 करोड़ यानी चीन से 30 लाख अधिक हो जाएगी। लेकिन इस आंकड़े से कुछ चिंताएं उभरती हैं। चीन में आबादी गिरने का प्रमुख कारण है एक काल-खंड में महिलाओं के प्रजनन में भारी गिरावट जिससे आज चीन की युवा शक्ति में अचानक कमी आ गई। चीन में सन् 1987 में 20 से 59 वर्ष आयु के लोगों का प्रतिशत 50 था, जो सन् 2011 में बढ़कर 61.5 हो गया । यही वह काल था जब चीन ने सांख्यिकी लाभ के जरिए जबरदस्त तरक्की की। अब वह चक्र उलटने जा रहा है। यह भारत के लिए अच्छा मौका है क्योंकि उसका सांख्यिकी लाभांश लेने का काल सन् 2018 से शुरू हो चुका है जो अगले 17 साल तक रहेगा। लेकिन यहां सवाल यह है कि लाभ केवल संख्या में ज्यादा युवाओं के खड़े होने से नहीं होगा। गर्भ से ही बच्चों को बेहतर पोषक भोजन और पैदा होने से 18 साल तक बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देना राज्य की पहली जिम्मेदारी होगी। फिर यह भी देखना होगा कि शिक्षा की दिशा क्या है? अभी तक सांख्यिकी लाभांश के चार साल बेकार चले गए हैं। बाल कुपोषण अभी भी विकराल समस्या बना हुआ है । अगर चीन की इस कमजोरी का लाभ उठाना है तो भारत की सरकार और समाज को दूरदृष्टि रखनी होगी।
Date:02-12-22
सरकार और जजों के बीच कब तक चलेगा टकराव?
विराग गुप्ता, ( लेखक और वकील )
अदालतों और जेलों की आम जनता से जुड़ी विफलताओं पर राष्ट्रपति ने संजीदगी से सवाल उठाए हैं। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति ने कहा विकसित होते भारत में जेलों के विस्तार की जरूरत क्यों है? द्रौपदी मुर्मू ने जब गरीबों की पीड़ा और लाचारी को व्यक्त किया तो सभागार में सन्नाटा छा गया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली स्वयं ही सजा बन गई है। इस लिहाज से निर्दोष कैदियों और तारीखों के चक्कर में फंसे करोड़ों लोगों के मानवाधिकारों के हनन के लिए जज भी जिम्मेदार हैं। विचार और जवाबदेही के इस चौराहे पर आम्बेडकर के बयान को दोहराना जरूरी है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे लागू करने वाले गलत होंगे तो संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाएगी।
कानूनी सुधार, क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल, न्यायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और कॉलेजियम में सुधार से जुड़ी सभी बातों का लक्ष्य सही और जल्द न्याय देना है। कानून मंत्री ने कॉलेजियम के खिलाफ गोलाबारी के लिए नए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल को ही क्यों चुना, इसकी अलग सियासत है। कोई सामान्य व्यक्ति अगर ऐसे बयान देता तो अदालत की अवमानना मानी जाती, लेकिन मंत्री के बयानों की अनदेखी हो रही है।
कानून मंत्री किरन रिजिजू ने कहा है कि एक ही संविधान की संतान होने के कारण जजों और मंत्रियों में लड़ाई ठीक नहीं है। लेकिन सास-बहू की तर्ज पर चल रही ‘तू-तू-मैं-मैं’ से साफ है कि संविधान की किसी को परवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए शेषन जैसे चुनाव आयुक्त की तर्ज पर जगमोहन सिन्हा जैसे निडर जजों की भी जरूरत है। जजों की निष्ठा व्यक्तियों की बजाय संविधान के प्रति हो, इसके लिए इन तीन बिंदुओं पर कॉलेजियम में सुधार के लिए राष्ट्रपति को पहल करनी चाहिए-
1. कॉलेजियम को संविधान का बुनियादी ढांचा मानने की बात पूरी तरह से गलत है। कोई भी प्रावधान, जो संविधान संशोधन या न्यायिक फैसले से शामिल किया गया हो, उसे संसद से पारित कानून से बदला भी जा सकता है। एनजेएसी कानून के निरस्त होने के सात साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दायर करने का कोई औचित्य नहीं दिखता। कॉलेजियम की सामंती, अपारदर्शी और मनमानी व्यवस्था को भी खत्म करना जरूरी है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत जजों की नियुक्ति का अधिकार सरकार को नहीं मिल सकता। इसलिए जजों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थान और सचिवालय बनाने के साथ न्यायपालिका के लिए स्वायत्त फंडिंग का सिस्टम बनना चाहिए।
2. एनजेएसी फैसले के अनुसार मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर (एमओपी) में बदलाव होने थे। पिछले सात सालों से पर्दे के पीछे कई चीफ जस्टिसों के साथ सरकार की तनातनी चल रही है। एमओपी में बदलाव के बगैर अपारदर्शी तरीके से जजों की मनमानी नियुक्ति पूरी तरह से गलत है। डेटा सुरक्षा कानून के बिल पर जनता से सुझाव मांगे गए उसी तर्ज पर एमओपी में बदलाव के लिए जनता और कानूनी समुदाय की राय लेकर नए नियमों को बनाकर लागू करना चाहिए।
3. नेता और मंत्री विफल हो जाएं तो 5 साल बाद जनता हटा सकती है। लेकिन महाभियोग की असंभव प्रक्रिया की वजह से पिछले 72 सालों में एक भी जज को नहीं हटाया गया । संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत जजों को शपथ पत्र देना होता है। उन प्रावधानों के अनुसार केएन गोविंदाचार्य ने डिस्क्लोजर एफिडेविट का मसौदा सुप्रीम कोर्ट और सरकार को दिया था। उसके अनुसार भाई-भतीजावाद खत्म करने के लिए जजों और नियुक्तिकर्ताओं के बीच सभी रिश्तों का खुलासा जरूरी है। इससे भ्रष्ट संस्कृति पर रोक लगने के साथ गलत एफिडेविट देने वाले जजों को सरल तरीके से हटाया जा सकेगा।
एमओपी में बदलाव और डिस्क्लोजर एफिडेविट सिस्टम को लागू करवाने के लिए अब देश की राष्ट्रपति को पहल करनी चाहिए। संवैधानिक मूल्य और जनता के हक के प्रति सजग पंच परमेश्वर जैसे जजों की नियुक्ति हो तो ओडिशा समेत देश के दूरस्थ इलाकों की जेलों में बंद लाखों बेगुनाह कैदियों के परिवारों में नया सवेरा आ सकता है।
एक बड़ा अवसर
संपादकीय
भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह जी-20 की आधिकारिक रूप से अध्यक्षता मिलना एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर का जितना उपयोग भारत का अंतरराष्ट्रीय कद बढ़ाने में किया जा सकता है, उतना ही विभिन्न समस्याओं पर विश्व समुदाय को एकजुट करने में भी। प्रधानमंत्री ने जी-20 के आगामी सम्मेलन को वसुधैव कुटुंबकम् की भावना के तहत आयोजित करने का संदेश देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका लक्ष्य दुनिया को दिशा देना और उन समस्याओं का समाधान एकजुट होकर खोजना है, जिनका विश्व समुदाय सामना कर रहा है। यह कठिन काम है, लेकिन पिछले कुछ समय में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की अहमियत बढ़ने के साथ जिस तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कद बढ़ा है, उससे यह आशा की जा सकती है कि वह मंदी की ओर बढ़ती दुनिया के बीच आर्थिक सहयोग कायम करने, ऊर्जा संकट को हल करने और आतंकवाद से वास्तव में दृढ़ता से लड़ने में सदस्य देशों के बीच ठोस सहमति बनाने में सफल होंगे। इसकी उम्मीद इसलिए की जाती है, क्योंकि भारत ने अपनी स्वतंत्र और दृढ़ विदेश नीति से विश्व के सभी प्रमुख देशों को प्रभावित किया है। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस और पश्चिमी देशों के बीच कायम तनातनी को यदि कोई देश खत्म कर सकता है तो वह भारत ही है। उचित यह होगा कि भारत इसके लिए प्रयत्न करे कि जी-20 सम्मेलन तक यूक्रेन युद्ध थम जाए। यह भारत के साथ विश्व समुदाय के भी हित में है। इससे जी-20 सम्मेलन की भी महत्ता बढ़ जाएगी और भारत की भी।
यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि जी-20 की अध्यक्षता देशवासियों को भारत के बढ़ते कद का आभास कराने में सहायक बनने के साथ उनमें गौरव की भावना का संचार करने का भी काम करेगी। शायद इसीलिए देश के 50 से अधिक शहरों में दो सौ से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा बनाई गई है। ये कार्यक्रम भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि और बेहतर बनाने के साथ देश के लोगों को यह संदेश देने का काम भी करेंगे कि भारत महाशक्ति बनने की राह पर है। निःसंदेह इस लक्ष्य की प्राप्ति तब और आसान होगी, जब देशवासी इसके प्रति आश्वस्त होंगे कि नए भारत का निर्माण हो रहा है। चूंकि यह स्पष्ट है कि जी-20 सम्मेलन को लेकर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम पर्यटन उद्योग को बल देने के साथ विश्व के प्रमुख देशों को भारतीय उत्पादों से परिचित कराने का भी काम करेंगे, इसलिए इस सम्मेलन के कुछ लाभों की गिनती अभी से की जा सकती है। जी-20 की मेजबानी देश के लिए एक ऐसी उपलब्धि है, जिसे विपक्षी दलों को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि विदेश नीति जुड़े विषय दल विशेष के नहीं, बल्कि समूचे देश के होते हैं।
Date:02-12-22
जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता पश्चिम
विवेक देवराय/आदित्य सिन्हा, ( देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और सिन्हा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में अपर निजी सचिव-अनुसंधान हैं )
मिस्र के शर्म अल-शेख में जलवायु सम्मेलन-सीओपी 27 संपन्न हो गया, लेकिन जलवायु परिवर्तन का मुद्दा ऐसा हो गया है जो हमेशा चर्चा में रहने लगा है। विकसित देश इसके लिए अक्सर विकासशील देशों को आड़े हाथों लेते हैं कि वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे। उच्च कार्बन उत्सर्जन को लेकर खासतौर से भारत और चीन जैसे देश उनके निशाने पर होते हैं। उनका यह रुख-रवैया हमें ‘व्हाइट मैन्स बर्डन’ यानी श्वेत-वर्णीय लोगों पर उस जिम्मेदारी के बोझ वाली श्रेष्ठताबोध की याद दिलाता है, जिसकी जड़ें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से जुड़ी हैं। स्पष्ट है कि पश्चिम अपने नैतिक श्रेष्ठता बोध के दंभ से बाहर आने को तैयार नहीं। वह इसे ‘सुझाव’ के रूप में प्रस्तुत करते हुए ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों को उपदेश देने में लगा है कि मानवता को बचाने के लिए उन्हें क्या करना है। गरीब देशों के लिए कार्बन स्पेस में गुंजाइश न देना और उन्हें उत्सर्जन में कटौती का उपदेश इसी मानसिकता का उदाहरण है।
पश्चिम चाहता है कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन को रोकने का बीड़ा उठाते हुए कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कटौती करें। जबकि वह कार्बन डाई आक्साइड और आर्थिक वृद्धि में मजबूत अंतर्संबंध को अनदेखा कर रहा है। इस तथ्यए का क्या कि पश्चिम का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन ग्लोबल साउथ से कहीं ज्यादा है। इन्हीं विकसित देशों ने अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ऊंची वृद्धि हासिल करने में दुनिया को प्रदूषित करने से गुरेज नहीं किया। वर्ष 1850 से 2011 तक ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन में 79 प्रतिशत हिस्सेदारी इन्हीं देशों की रही। पश्चिमी खेमे ने उन मुद्दों पर तो मुखरता दिखाई, जिनसे उस पर सीधे असर पड़ता, जबकि गरीब देशों की आवश्यकताओं को लेकर उसका रवैया हीलाहवाली भरा रहा। यही पश्चिमी देश उन देशों के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें शर्मसार करने के अभियान में लगे हैं, जो इनके श्रेष्ठता बोध से भरे सुझावों को नहीं मानते।
जलवायु परिवर्तन की चुनौती को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है मानो यही मानवता के समक्ष एकमात्र संकट है। दुनिया अभी भी महामारी से उबर रही है। कुपोषण अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। यूक्रेन-रूस संकट से वैश्विक स्तर पर बढ़ रही महंगाई ने कई देशों को मंदी की राह पर धकेल दिया है। हालांकि भारत इस मामले में अपवाद है, जहां अर्थव्यवस्था अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में और यहां तक कि विकसित देशों से भी अपेक्षाकृत बेहतर कर रही है। इस तथ्य को भी नहीं नकारा जा सकता कि आर्थिक विकास की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवश्म ईंधन से हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण में कुछ समय लगेगा। शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारत को कोयला-आधारित तापीय बिजली संयंत्रों से हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख करना होगा।
भारत जैसे देश के लिए यह आसान नहीं होगा, जहां अधिकांश ऊर्जा तापीय बिजली संयंत्रों से प्राप्त होती है। नि:संदेह जलवायु परिवर्तन की चुनौती वास्तविक है। विकासशील देश और द्वीपीय राष्ट्र तो जलवायु संबंधी आपदाओं का ध्वंस भी झेल रहे हैं। ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या कार्बन उत्सर्जन का ठीकरा विकासशील देशों पर फोड़कर उसमें कटौती का पूरा दारोमदार उन्हीं देशों पर लाद दिया जाए और पश्चिमी देश अंतहीन सौदेबाजी में लगे रहें? वास्तविकता यही है कि विकसित देशों ने पिछली शताब्दी में जलवायु को विकृत करने का जो काम किया, उसकी भरपाई में वे पूरी तरह विफल रहे हैं।
विदेशी पूंजी के बिना विकासशील देशों के लिए हरित ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाना मुश्किल होगा। यह पूंजी भी सुगमता और रियायत के साथ उपलब्ध करानी होगी। जलवायु वित्तपोषण के लिए सीमित विकसित देशों ने 2020 से हर साल गरीब देशों को 100 अरब डालर उपलब्ध कराने पर सहमति जताई थी, लेकिन जलवायु वित्तपोषण पर स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह के अनुसार 2020 में भी 100 अरब डालर की वार्षिक प्रतिबद्धता का यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। विकसित देशों ने फिर से वादा किया कि कम विकसित देशों को 2020 से सालाना 100 अरब डालर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक उसी समय संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि इस दिशा में कहीं अधिक राशि की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन पर गठित संयुक्त राष्ट्र अंतरसरकारी पैनल के अनुसार यदि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करना है तो हर साल 1.6 से 3.8 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की आवश्यकता होगी। यह पूरी तरह विकसित दुनिया के उसी दस्तूर की भांति है, जिसमें वह किसी बात का वादा तो करता है, लेकिन उस पर खरा नहीं उतरता। हाल के दौर में उसका यह रुख-रवैया उजागर होता रहा है।
सीओपी-27 में नुकसान और क्षतिपूर्ति लिए विशिष्ट कोष बनाने का निर्णय हुआ है। जलवायु न्याय वार्ताओं में इसे विकासशील देशों के लिए बड़ी सफलता माना जा सकता है। यह विकसित दुनिया द्वारा उनके पापों की स्वीकृति से कम नहीं है। यदि इस कोष की व्यवस्था आदर्श रूप में आकार ले पाती है तो इससे उन संवेदनशील देशों को बहुत लाभ पहुंचेगा, जिनका जलवायु संकट को बढ़ाने में तो उतना योगदान नहीं, जितना उन्हें उसका कोप झेलना पड़ रहा है। हालांकि वादे से मुकरने का विकसित देशों का पुराना रिकार्ड है, जो 100 अरब डालर के संकल्प में भी दिखा। इसके बावजूद विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन घटाने के प्रयास जारी रखने चाहिए। भारत ने 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली गैर-जीवाश्म ईंधनों से बनाने का लक्ष्य रखा है। विकसित देशों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जलवायु परिवर्तन के इस बिल की भरपाई तो उन्हीं को करनी चाहिए, जिन्होंने अतीत से भारी प्रदूषण फैलाया। सतत जलवायु वित्तपोषण वास्तव में ‘विकसित देशों’ का दायित्व है और इसका बोझ निम्न एवं मध्यम आय और विकासशील देशों में भी सबसे आखिरी पायदान पर रहने वाले देशों पर नहीं डाला जाना चाहिए।
 Date:02-12-22
Date:02-12-22
ठोस पुनर्विचार की जरूरत
संपादकीय
एक स्वागतयोग्य पहल में सरकार ने अपनी प्रमुख फसल बीमा योजना-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में किसान समर्थक बदलावों की पेशकश की है। ऐसा जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि में आ रही दिक्कतों के कारण किया जा रहा है। यह कदम जरूरी माना जा रहा है क्योंकि यह फसल बीमा योजना 2018 और 2020 में किए गए सुधारों के बावजूद राज्य सरकारों और किसानों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी।आश्चर्य नहीं कि इस योजना का क्रियान्वयन करने वाले राज्यों की तादाद में कमी आई है और वह 2018 के 22 से घटकर अब 19 रह गई है। साथ ही इस योजना को अपनाने वाले किसानों की तादाद भी 2.16 करोड़ से घटकर 1.53 करोड़ रह गई है। अधिकांश राज्य सरकारें वित्तीय तंगी से जूझ रही हैं और उनके लिए इस योजना में अपने हिस्से की सब्सिडी चुकाना मुश्किल है। किसानों को भी यह योजना बहुत अधिक आकर्षक नहीं लग रही है।
बीमा कंपनियां जो हर्जाना देती हैं वह अक्सर बहुत कम होता है और देर से मिलने के कारण बहुत मददगार भी नहीं साबित होता। किसान संगठनों समेत पीएमएफबीवाई के आलोचक बीमा कंपनियों पर इल्जाम लगाते हैं कि वे इस योजना से जमकर लाभ कमा रही हैं लेकिन वे कंपनियां इन आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहती हैं कि किसान बीमा कम मुनाफे वाला कारोबार है क्योंकि खेती जैसी गतिविधि में बहुत सारे जोखिम शामिल होते हैं। यही कारण है कि कुछ कंपनियों ने बीमा कवर देना भी बंद कर दिया है।
पीएमएफबीवाई निस्संदेह सन 1970 के दशक से अब तक आजमाई गई फसल बीमा योजनाओं में सबसे अच्छी और व्यापक योजना है। इस योजना में बोआई से पहले और फसल कटाई के बाद के नुकसान को भी शामिल किया गया है और इसमें बीमित राशि की कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसमें कई ढांचागत खामियां हैं जो इसकी क्षमता को प्रभावित करती हैं। हालांकि कागज पर यह केंद्र सरकार की योजना है जिस पर प्रधानमंत्री का ठप्पा भी है लेकिन इसकी आधी लागत राज्यों को साझा करनी होती है। इसका क्रियान्वयन भी सरकारी और निजी उपक्रमों के हाथों में होता है। इसकी वजह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। ऐसे में समस्या का हल इस बात में निहित है कि या तो इसे पूरी तरह केंद्रीय योजना बना दिया जाए और सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करे या फिर इसे पूरी तरह राज्यों पर छोड़ दिया जाए क्योंकि संविधान के तहत तो वैसे भी कृषि राज्य का विषय है। उस स्थिति में राज्य किसानों को हर्जाना देने का निर्णय ले सकते हैं या फिर वे हालात के अनुसार बीमा मॉडल बना सकते हैं जो किसानों को स्वीकार्य हो। किसी भी स्थिति में राज्य खेती के जोखिम का आकलन करने के लिहाज से बेहतर स्थिति में होंगे और इसलिए फसल के नुकसान का भी सही आकलन कर पाएंगे। स्थानीय कृषि-पारिस्थितिकी हालात के कारण फसल नुकसान भी अलग-अलग होता है। दावों के देर से निपटान और नुकसान की तुलना में अपर्याप्त भुगतान की समस्या को भी हल करने की आवश्यकता है। हालांकि किसानों के दावों के लिए समय के मानक पीएमएफबीवाई में भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं लेकिन अक्सर उनकी अनदेखी कर दी जाती है। आधुनिक तकनीक मसलन फसल नुकसान की जानकारी के लिए डिजिटल ऐप, दावों की पुष्टि के लिए सैटेलाइट इमेजरी और क्षतिपूर्ति चुकाने के लिए प्रत्यक्ष नकदी स्थानांतरण आदि का इस्तेमाल करके इस पहलू को आसानी से हल किया जा सकता है। ऐसे में जरूरत यह है कि पीएमएफबीवाई में कुछ समुचित ढांचागत और प्रक्रियागत बदलाव किए जाएं ताकि यह बीमा कंपनियों के लिए उचित साबित हो और किसानों के लिए भी वित्तीय लाभ लेकर आए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह सुविचारित योजना भी कमजोर साबित होगी।
अमीरी का चुनाव
संपादकीय

अब इस तथ्य को आम मतदाता भी जैसे स्वीकार कर चुका है कि एक बार चुनाव जीतने के बाद जन प्रतिनिधि अचानक फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि जन प्रतिनिधियों को वेतन इतना अधिक मिलता है कि पांच सालों में उनकी जमा पूंजी में करोड़ों की बढ़ोतरी हो जाती है। मगर न तो उन पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले दर्ज किए जाते हैं और न उनकी पार्टी उनके खिलाफ कोई कदम उठाती है। यह कौन पूछेगा कि आखिर पांच सालों में उनकी आमदनी इतनी कैसे हो जाती है कि उनकी संपत्ति में अचानक बढ़ोतरी हो जाए। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि इस तरह की संपत्ति भ्रष्टाचार के जरिए जमा होती है। दिल्ली नगर निगम पार्षदों को विकास कार्य के लिए हर साल एक तय रकम जारी की जाती है। उस रकम के आबंटन में ठेकेदारों से कमीशनखोरी जगजाहिर है। इसके अलावा भी अतिक्रमण, बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण कराने आदि के लिए उगाही के तथ्य प्रकट हैं। इस चुनाव में विपक्षी राजनीतिक दल इसका खुलेआम आरोप लगाते फिर रहे हैं। फिर यह भी छिपी बात नहीं है कि जन प्रतिनिधि और अधिकारी भ्रष्टाचार से जुटाया बहुत सारा धन और संपत्ति अपने नाम से नहीं रखते। इस तरह उनकी अघोषित संपत्ति का भी अंदाजा लगाया जा सकता है।
विचित्र है कि दिल्ली नगर निगम में वर्षों से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। उसके कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता, जिसे लेकर वे जब-तब प्रदर्शन पर उतर आते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं। नगर निगम के स्कूलों, मुहल्लों की गलियों, सड़कों, उनमें रोशनी, सार्वजनिक शौचालयों आदि की दशा दयनीय बनी हुई है। साफ-सफाई के मामले में हर रोज शिकायतें आती रहती हैं। कचरा प्रबंधन तो इस बार के चुनाव में प्रमुख मुद्दा बन चुका है। इन सब पहलुओं पर ध्यान देने के बजाय निगम पार्षदों का ध्यान अपनी जेबें भरने पर लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। मगर सवाल है कि क्या उन पार्षदों के खिलाफ उनकी पार्टियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।
निगाहें भारत की तरफ
संपादकीय
हाल के वर्षों में खासकर केंद्र में नरेन्द्र मोदी के सत्तारूढ़ होने के बाद से भारत की वैश्विक मंच पर स्वीकार्यता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ी है। जी-20 की अध्यक्षता भारत को मिलने से निःसंदेह देश की ताकत में इजाफा हुआ है। चूंकि जी-20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी, लिहाजा भारत की भूमिका यहां ज्यादा वड़ी हो जाती है। देश-दुनिया का चरित्र आहिस्ता-आहिस्ता वदल रहा है। पहले की कूटनीति और अव की कूटनीति में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। जो देश कभी अपने भारत जैसे विकासशील देश को कमतर आंकते थे, अब वो भारत को वैश्विक तौर पर अग्रणी भूमिका में देखते हैं। भारत के प्रति उन देशों की सोच में आश्चर्यजनक बदलाव आया है।
शायद यही भारत की बढ़ती हनक और उसकी जिम्मेदार राष्ट्र का द्योतक है। वहरहाल जी-20 के लिए हमारी थीम है ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य।’ यह महज एक नारा नहीं है। ये मानवीय परिस्थितियों में उन वदलावों को ध्यान में रखता है, जिनकी सराहना करने में हम विफल रहे हैं। साफ है कि हमारी ओर विश्व उम्मीदों की नजर से देख रहा है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सम्मानित शख्सियतों ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन, उनकी सोच, उनकी प्राथमिकताओं और मंतव्यों पर विश्वास जताया है। उन्हें परम भरोसा है कि भारत ही आने वाले कल का सूरज है, जो दुनिया के दुख-दर्द, उनकी दुश्वारियों आदि को समावेशी तरीके से हल करेगा। सामूहिक निर्णय लेने की सवसे पुरानी ज्ञात परंपराओं वाली सभ्यता होने के नाते भारत दुनिया में लोकतंत्र के मूलभूत डीएनए में योगदान देता है। स्पष्ट है कि भारत जी-20 की अध्यक्षता के दरम्यान अपने अनुभव, ज्ञान और प्रारूप को दुनिया की समस्याओं को खत्म करने का सजग प्रयास जरूर करेगा । रूस- यूक्रेन के वीच लगातार उलझते संबंध, यूरोपीय देशों और रूस के बीच कड़वाहट, भारत का अपने पड़ोसी देश विशेषकर पाकिस्तान और चीन के साथ असहज रिश्ता दुनिया में अमन बहाली की राह में बड़े अवरोधक हैं। चुनांचे, भारत की जिम्मेदारी भी ज्यादा हो जाती है। अलवत्ता, भारत के गौरवशाली अतीत की छाया आगे भी दुनिया को भावी संकट से उवारने में पीछे नहीं हटेगी।
