
01-06-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:01-06-23
Date:01-06-23
It’s A Judgment Call
Ugandan law and Japanese court judgment show why only SC can greenlight same-sex marriage
TOI Editorials
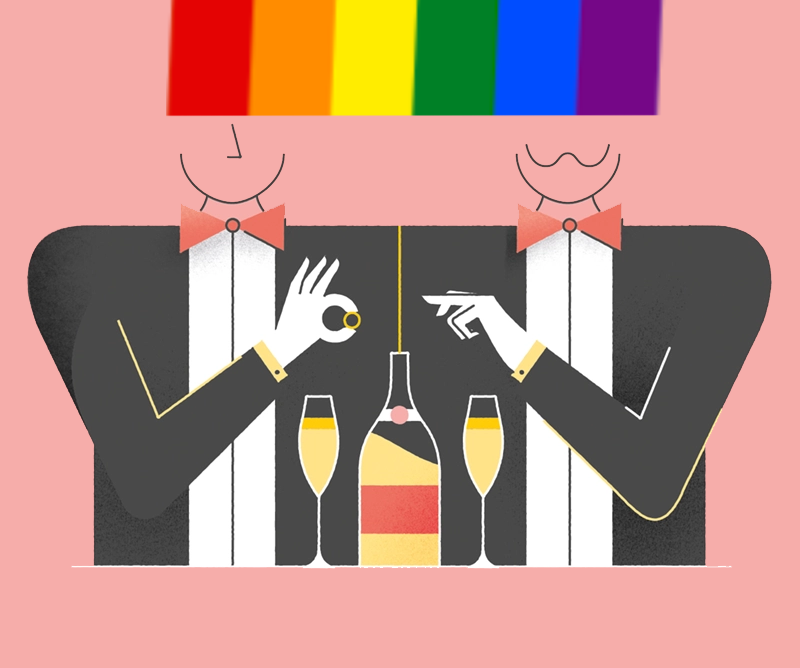
Uganda’s new law is a standout example of anti-LGBTQ bigotry, even in a continent largely hostile to their rights. It imposes life imprisonment for anyone who has been in a consensual same-sex sexual encounter, and the death penalty for ‘aggravated homosexuality’, by which it means sexual contact with children and other vulnerable groups – as though they are all shades of the same thing. This law is a drastic violation of human rights, it makes ordinary loving and living impossible for LGBTQ persons.
Until five years ago, India was also among the former British colonies that used the law to harass, humiliate and deny consenting LGBTQ adults their rights. In 2018, Section 377 was read down, affirming the right to equality and non-discrimination, and the Puttuswamy judgment entrenched privacy as part of every citizen’s life and liberty, which means that the state cannot encroach into the individual domain, which includes consensual domestic and sexual arrangements. The right to same-sex marriage, being heard by the Supreme Court, should flow out of these judgments. The right to love and marry, have the protections and responsibilities of a family, cannot be denied by the state to any adult citizen. And only the courts can make this happen.
Doth Protest Too Much About Protests?
ET Editorials
Article 19(1)(b) of the Constitution provides all citizens the right to assemble peacefully and without arms. It also provides restrictions that are ‘sensible’ and ‘obligatory in the welfare of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morals, or in relation to the disdain of court, offence, or incitement to an offence’. In other words, if the first half of the law provides the letter, the second half provides the spirit. For the latter to comply with the former, one needs to obtain a ‘no objection certificate’ (NOC) from the police station within the jurisdiction of which one plans the public gathering of protest. Indeed, it is the decision — marzi (wish), if you will — of the authorities to allow or revoke gatherings of this nature by invoking Section 144 of the Criminal Procedure Code (CrPC): curfew.
Going by this letter of law, gatherings per se can, indeed, cause ‘annoyance’ to ‘any person’ and be the source of ‘disturbance of public tranquillity’. By this reading, protests, even in a democratic space, are up for subjective hyper-scrutiny and cherry-picking. In other words, every protest can be deemed unlawful if the authorities choose to see it as being so.
By their very nature, ‘peaceful’ public protests are disruptive, anti-status quo-ist. For the allowance of such a democratic right to have any practical meaning, it would be wise to be more specific and detailed in law to define what amounts to ‘annoyance’ and ‘disturbance of public tranquillity’. All protests don’t take place in ‘Tiananmen Squares’. And they certainly don’t amount to challenging the ‘welfare of the sovereignty and integrity of India, the security of the State’.
Status quo in Turkey
Erdoğan must right the wrongs of the past and offer a new inclusive beginning
Editorial
When Recep Tayyip Erdoğan’s Justice and Development Party (AKP) came to power in 2002, riding widespread resentment against the establishment amid economic woes, he was a political outsider — an Islamist in a system dominated by Kemalist secularists. Twenty years later, Mr. Erdoğan is the establishment — the military, traditionally the guardian of the old order, is under his thumb, institutions are at his command and the AKP, with close links to the ulema, remains a hegemonic political machine. But the economic and political situation of 2023 is comparable with that of 2002. Faced with a deepening economic crisis and accusations of backsliding democracy and freedoms, there has been widespread resentment against his long reign. The Opposition united to capitalise on this anger and managed to deny him a first round victory on May 14, but in Sunday’s run-off, he won 52.1% of the vote share, against Kemal Kılıçdaroğlu’s 47.9%. Mr. Kılıçdaroğlu has accepted the outcome, but called the election process “the most unfair in years”. He has a point. Mr. Erdoğan and his allies controlled the big media, shaping the information flow. State institutions, including the religious directorate (Diyanet), which controls mosques and appoints Imams, amplified the AKP propaganda. The President accused the Opposition of having ties with “terrorists” as a mainstream Kurdish party was backing his rival. Mr. Kılıçdaroğlu, a former bureaucrat from the minority Alevi community, led a spirited campaign, but failed to overcome the AKP’s Islamist populism.
Mr. Erdoğan, arguably the most powerful Turkish leader since Mustafa Kemal ‘Atatürk’, has reshaped the country’s polity and society over the past 20 years. Kemal Atatürk, who abolished the Ottoman Caliphate and secularised Turkey, saw the clergy as a threat to his vision for the country. Tensions between Kemalism and Islamism have always been there in Turkey’s modern history. But until Mr. Erdoğan’s rise to power, no Islamist leader had managed to upend the system. While doing so, he amassed powers, rewrote the Constitution, turning it into an executive presidency, got himself elected as the all-powerful President, stifled dissent, stepped up the war against Kurdish rebels, and jailed political rivals. Yet, this election was his biggest challenge. That he had to go into the second round, and with a lead of just three points, should remind him that Turkish society remains polarised. The battered economy needs urgent attention. A new term is an opportunity for Mr. Erdoğan, whose legacy has already been marred by his authoritarian tendencies and mismanagement of the economy, to right the wrongs and offer a new inclusive beginning. But it is unclear whether Turkey’s Islamist leader is ready for such a change.
Date:01-06-23
A parliamentary democracy or an executive democracy
Even as the new Parliament has been inaugurated, what is overlooked is the increasing subordination of ‘Parliament’ in India’s ‘parliamentary democracy’
Gautam Bhatia is a Delhi-based lawyer
Last week, a new Parliament building was inaugurated with both fanfare and controversy. In particular, the exclusion of the President of India — the formal head of the executive — from the inauguration, and the symbolism around the Sengol — a sceptre originally used to signify the transfer of power between Chola rulers — generated significant debate. Submerged beneath this debate, however, is an overlooked fact: the increasing subordination of the “Parliament” in India’s “parliamentary democracy.”
Parts of this story are familiar: we know that Bills are passed with minimal or no deliberation. We know that Parliament sits for fewer and fewer days in a year, and parliamentary sessions are often adjourned. We know that presidential ordinances have become a parallel if not dominant form of law-making.
By constitutional design
It is tempting to attribute all of this to unscrupulous or callous politicians. What that misses, however, is the understanding that the growing irrelevance of Parliament is not because of individual actions but a matter of constitutional design. In other words, the Indian Constitution, by its very structure, facilitates and enables the marginalisation of Parliament, and the concentration of power within a dominant executive.
How does this happen? Consider the various safeguards that parliamentary democracies generally tend to put in place against executive dominance or abuse. First, in order to enact its agenda, the executive must command a majority in Parliament. This opens up the space for intra-party dissent, and an important role for ruling party parliamentarians — who are not members of the cabinet — to exercise a check over the executive. Occasionally, ruling party backbenchers can even join forces with the Opposition to defeat unpopular Bills (as was the case with various Brexit deals in the U.K. House of Commons between 2017 and 2019). Second, the Opposition itself is granted certain rights in Parliament, and certain limited control over parliamentary proceedings, in order to publicly hold the executive to account. Third, the interests of Parliament against the executive are meant to be represented by the Speaker, a neutral and independent authority. And fourth, certain parliamentary democracies embrace bicameralism: i.e., a second “Upper House” that acts as a revising chamber, where interests other than those of the brute majority are represented (in our case, that is the Rajya Sabha, acting as a council of states).
When these features function as they should, it becomes very difficult for the executive to ride roughshod over Parliament and, in turn, opens up space for Parliament to act as the deliberative and representative body that it is meant to be.
A dilution, erasure
In India, however, each of these features has been diluted or erased over the years.
First, the possibility of intra-party dissent within Parliament has been stamped out by virtue of the Tenth Schedule to the Constitution, popularly known as the “anti-defection law”. Introduced through a constitutional amendment in 1985, the Tenth Schedule penalises disobedience of the party whip with disqualification from the House altogether. Ironically, as recent events have more than amply demonstrated, the Tenth Schedule has failed to fulfil the purpose for which it was enacted, i.e., to curb horse-trading and unprincipled floor-crossing. What it has done, however, is to strengthen the hand of the party leadership — which, in the case of the ruling party, is effectively the cabinet/executive — against its own parliamentarians. Intra-party dissent is far more difficult when the price is disqualification from Parliament.
Second, right from its inception, the Indian Constitution did not carve out any specific space for the political Opposition in the House. There is no equivalent, for example, of Prime Minister’s questions, where the Prime Minister has to face direct questioning of their record from the Leader of the Opposition as well as by other politicians. In other words, the manner of proceedings in Parliament are under the complete control of the executive, with no real constitutional checks upon how that control is exercised.
Third, this is exacerbated by the fact that the Speaker, in our system, is not independent. The Speaker is not required to give up membership of their political party, and is not constitutionally obligated to act impartially. This has led to an increasing trend, at both the central and the State levels, of Speakers acting in a blatantly partisan manner in order to advance the interests of the executive over the interests of the House. Not only does this affect the quality of the deliberations in the lower house (as the Speaker has control over the conduct of the House) but it also has a knock-on effect on the Upper House: as has been seen of late, when the ruling party wishes to avoid effective scrutiny in the Rajya Sabha over Bills, the Speaker simply classifies the Bill as a “money bill”, thus depriving the Rajya Sabha of the right to make amendments. This was seen most vividly in the case of the Aadhaar Act, where Rajya Sabha scrutiny was avoided in this precise manner, and many important, rights-protecting amendments could not be passed.
Role of the Upper House
Fourth, the role of the Upper House is undercut not only by the Speaker’s misclassification of Bills but also by the constitutionally-sanctioned ordinance making power. An ordinance is nothing more than executive legislation; and while, in theory, it is meant to be used only for an emergency, while Parliament is not in session, in practice, it is used as a parallel process of law-making, especially when the executive wants to bypass the Upper House altogether, at least for a period of time, and create a fait accompli.
When we put all of this together, what emerges is a picture where the only effective check upon the executive is one where the electorate has thrown up a fractured mandate and the ruling party is forced to govern in a coalition with allies with whom it does not always see eye-to-eye. In such a scenario, coalition partners can exercise something of a check upon the executive in Parliament.
However, when there is a single, majority ruling party, whether at the Centre or in the States, there is very little that Parliament can do. The anti-defection law wipes out intra-party dissent. The political Opposition’s scope for participation depends upon the discretion of the executive. Partisan Speakers further ensure that the executive is insulated from public embarrassment at the hands of the Opposition, by controlling the debate. And the Upper House is taken out of the equation, either by the misclassification of money Bills or by the use of ordinance power.
It is no wonder, then, that the quality of parliamentary deliberations has declined: it is simply a mirror of Parliament’s own structural marginalisation under the Constitution. Instead, what we have is greater and greater executive power: a situation that resembles presidential systems with strong executives, but without the checks and balances and veto points that those systems have; in effect, the worst of all worlds.
Therefore, even as the new Parliament is inaugurated, the urgent question that we must ask is whether in formal terms, India can continue to be called a parliamentary democracy, or whether we have gradually morphed into an executive democracy. And if, indeed, we want to return to parliamentarianism, what manner of constitutional changes and reforms that it would require.
आर्थिक असमानता हो तो विकास का पैमाना बदलें
संपादकीय
जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद ) देश के सभी उत्पादों और सेवाओं की मार्केट वैल्यू का कुल योग होती है। यह सच है कि भारत जीडीपी में ब्रिटेन को पछाड़ कर पांचवें स्थान पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के पैमाने पर दोनों देशों में 20 गुना अंतर है। इंडोनेशिया की प्रति व्यक्ति आय दूनी, ब्राजील की चार गुनी और चीन की छह गुनी है। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक में हम पिछले 33 वर्षों में 130-135वें स्थान पर ही खड़े हैं। देश में पिछले 12 वर्षों से गरीबी का सांख्यिकी आकलन नहीं किया गया। वर्ल्ड बैंक के 2022 के अध्ययन अनुसार सन् 2019 तक 13.70 करोड़ लोग 46 रुपए प्रति दिन और 61.20 करोड़ लोग 78 रुपए प्रति दिन पर गुजारा कर रहे थे। कोरोना के बाद गरीबों की संख्या ढाई से पांच करोड़ और बढ़ गई। वहीं विश्व बैंक की पिछले वर्ष की रिपोर्ट भारत को सबसे असमानता वाले कुछ देशों में शुमार करती है, जहां ऊपर के 10% लोगों की आय नीचे के 50% लोगों से 22 गुना ज्यादा है। दरअसल यह आर्थिक असमानता सन 1990 के तथाकथित आर्थिक उदारीकरण की देन है, यानी किसी एक सरकार या काल की नहीं बल्कि गलत आर्थिक नीतियों से पैदा हुई है। आज जरूरत जीडीपी में वृद्धि देखकर खुश होने की नहीं बल्कि आर्थिक असमानता कम करने वाली नीतियां बनाने की है।
हस्तक्षेप करे सरकार
संपादकीय
उद्घाटन के दिन यानी 28 मई को जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान अपना विरोध जताने के लिए नये संसद भवन तक नहीं पहुंच पाए। पुलिस बल के चलते उनके समर्थक किसान भी दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाए। पुलिस ने पहलवानों सहित अनेक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और धरना स्थल जंतर मंतर भी खाली करा दिया। इस कार्रवाई से निराश – हताश पहलवानों ने अपने-अपने मैडल गंगा में प्रवाहित करने की घोषणा कर दी। ऐसा करने के लिए वे हरिद्वार में गंगा तट पर पहुंच भी गए, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत के हस्तक्षेप से उन्होंने मैडल विसर्जन का कार्यक्रम तात्कालिक तौर पर स्थगित कर दिया है। नरेश टिकैत ने पहलवानों से पांच दिन का समय मांगा है यानी परोक्ष तौर पर उन्होंने सरकार को पांच दिन का समय दिया है कि वह वृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करे अन्यथा किसी बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। दूसरी ओर, पुलिस ने जो रुख अपनाया है, उससे नहीं लगता कि अगले पांच दिनों में वृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो सकेगी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि गिरफ्तारी होगी भी या नहीं। यानी सरकार और पहलवानों के बीच प्रतिरोध की जो स्थिति बनी है, वह टूटती नहीं दिख रही है। पांच दिन वाद आंदोलनकारी क्या कदम उठाएंगे और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन जो हो रहा है, वह किसी भी सूरत अच्छा नहीं हो रहा है। इधर, देश के भीतर मोदी सरकार की छवि खराव हो रही है और देश के बाहर भारत की । यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पहलवानों की गिरफ्तारी की निंदा की है। और 45 दिन के अंदर भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव कराने की चेतावनी दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहलवानों का आंदोलन मोदी विरोधियों का अखाड़ा वन गया है। हर मोदी विरोधी तत्व इस आंदोलन के जरिए अपनी रणनीति को आगे बढ़ाता दिख रहा है, लेकिन मात्र इस बहाने से कि पहलवानों का आंदोलन मोदी विरोधियों द्वारा प्रेरित है, सरकार अपने दायित्व से नहीं बच सकती। 28 मई को जिस तरह पहलवानों के साथ वल प्रयोग किया गया उससे सामान्य लोगों की नैतिक चेतना पहलवानों के साथ है, और सरकार के रवैये से जनसामान्य बेहद आहत है। इसलिए समय रहते इस समूची परिस्थिति का संज्ञान लिया जाना चाहिए और इससे पहले कि सरकार की छवि को ध्वस्त करने वाली कोई बड़ी घटना घटे, इस स्थिति का समुचित समाधान निकाला जाना चाहिए।
Date:01-06-23
खेती पर काबिज होने का खेल
भारत डोगरा
हाल के वर्षो में किसानों के संकट का एक बड़ा कारण है कि उनकी आत्मनिर्भरता और स्वावलंबिता में भारी गिरावट आई है। वे कृषि की नई तकनीकों को अपनाने के साथ रासायनिक कीटनाशक, खरपतवारनाशक, रासायनिक खाद, बाहरी बीजों और उपकरणों पर बहुत निर्भर हो गए हैं।
जहां जमीनी स्तर पर किसान इन अनुभवों से गुजर रहे थे, वहां बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्तर पर ऐसे प्रयास भी चल रहे थे कि किसानों पर अपना नियंत्रण और बढ़ा लिया जाए। इस नियंत्रण को बढ़ाने का प्रमुख साधन बीज को बनाया गया क्योंकि बीज पर नियंत्रण होने से पूरी खेती-किसानी पर नियंत्रण हो सकता है। इसलिए बड़ी कंपनियों ने बीज क्षेत्र में पैर फैलाने आरंभ किए। जो बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आई, वे पहले से कृषि रसायनों विशेषकर कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों आदि के उत्पादन में लगी हुई थीं। इस तरह बीज उद्योग और कृषि रसायन उद्योग एक ही तरह की कंपनी के हाथ में केंद्रीकृत होने लगे। इसी समय के आसपास जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ महत्त्वपूर्ण अनुसंधान हो रहे थे और वैज्ञानिक विशिष्ट गुणों वाले जीन को एक जीव से दूसरे जीव में प्रवेश दिला कर जीवन के विभिन्न रूपों को, उनके गुणों को बदलने की क्षमता प्राप्त कर रहे थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त फसलों को संक्षेप में जीएम (जेनेटिकली मोडीफाइड) फसल कहते हैं।
सामान्यत: एक ही पौधे की विभिन्न किस्मों से नई किस्में तैयार की जाती रही हैं जैसे गेहूं की दो किस्मों से गेहूं की एक नई किस्म तैयार कर ली जाए पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी भी पौधे या जंतु के जीन या आनुवांशिक गुण का प्रवेश किसी अन्य पौधे या जीव में करवाया जाता है जैसे आलू के जीन का प्रवेश टमाटर में करवाना या सुअर के जीन का प्रवेश टमाटर में करवाना या मछली के जीन का प्रवेश सोयाबीन में करवाना या मनुष्य के जीन का प्रवेश सुअर में करवाना आदि। जीएम फसलों के विरोध का एक मुख्य आधार यह रहा है कि ये फसलें स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं तथा यह असर जेनेटिक प्रदूषण के माध्यम से अन्य सामान्य फसलों और पौधों में फैल सकता है। अब इस बारे में व्यापक सहमति है कि इन फसलों का प्रसार होने पर ट्रांसजेनिक प्रदूषण से बचा नहीं जा सकता। इसलिए जीएम फसलों और गैर-जीएम फसलों का सहअस्तित्व नहीं हो सकता। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जीएम फसलों की सुरक्षा या सेफ्टी प्रमाणित नहीं हो सकी है। इसके विपरीत पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं, जिनसे इन फसलों की सेफ्टी या सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। यदि इनकी उपेक्षा की गई तो स्वास्थ्य और पर्यावरण की क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, जिसे फिर ठीक नहीं दिया जा सकता। जीएम फसलों को अब दृढ़ता से रिजेक्ट कर देना चाहिए, अस्वीकृत कर देना चाहिए। जेनेटिक प्रदूषण का मूल चरित्र ही ऐसा है। वायु और जल प्रदूषण की गंभीरता पता चलने पर इनके कारणों का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, पर जेनेटिक प्रदूषण जो पर्यावरण में चला गया हो, वह हमारे नियंतण्रसे बाहर हो जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रचार कई बार इस तरह किया जाता है कि किसी विशिष्ट गुण वाले जीन का ठीक-ठीक पता लगा लिया गया है और इसे दूसरे जीव में पंहुचा कर उसमें वही गुण उत्पन्न किया जा सकता है किंतु हकीकत इससे अलग और कहीं अधिक पेचीदी है।
कोई भी जीन केवल अपने स्तर पर या अलग से कार्य नहीं करता अपितु बहुत से जीनों के एक जटिल समूह के एक हिस्से के रूप में कार्य करता है। इन असंख्य अन्य जीनों से मिलकर और उनसे निर्भरता में ही जीन के कार्य को देखना-समझना चाहिए, अलगाव में नहीं। एक ही जीन का अलग-अलग जीवों में काफी भिन्न असर होगा क्योंकि उनमें जो अन्य जीन हैं, वे भिन्न हैं। विशेषकर जब एक जीव के जीन को काफी अलग तरह के जीव में पंहुचाया जाए तो, जैसे मनुष्य के जीन को सुअर में, तो इसके काफी नये और अप्रत्याशित परिणाम होने की संभावना है। इतना ही नहीं, जीनों के समूह का किसी जीव की अन्य शारीरिक रचना और बाहरी पर्यावरण से भी संबंध है। जिन जीवों में वैज्ञानिक विशेष जीन पंहुचाना चाह रहे हैं, उनसे अलग जीवों में भी इन जीनों के पंहुचने की संभावना रहती है, जिसके अनेक अप्रत्याशित परिणाम और खतरे हो सकते हैं।
बाहरी पर्यावरण जीन के असर को बदल सकता है और जीन बाहरी पर्यावरण को इस तरह प्रभावित कर सकता है, जिसकी संभावना जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करने वालों को नहीं थी। एक जीव के जीन दूसरे जीव में पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक जिन तरीकों का उपयोग करते हैं, उनसे अप्रत्याशित परिणामों और खतरों की संभावना और बढ़ जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अधिकांश महत्त्वपूर्ण उत्पादों के पेटेंट बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास हैं और वे अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए इस तकनीक का जैसा उपयोग करती हैं, उससे इस तकनीक के खतरे और बढ़ जाते हैं। कृषि और खाद्य क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी मात्र लगभग छह-सात बहुराष्ट्रीय कंपनियों (और उनकी सहयोगी या उप-कंपनियों) के हाथ में केंद्रित हैं। इन कंपनियों का मूल आधार पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका में है। कुछ समय पहले देश के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर पुष्प भार्गव का निधन हुआ है। वे सेंटर फॉर सेलयुलर एंड मॉलीक्यूलर बॉयलाजी, हैदराबाद के संस्थापक निदेशक और नेशनल नॉलेज कमीशन के उपाध्यक्ष रहे। जीएम फसलों के विरुद्ध उनकी चेतावनी महत्त्वपूर्ण है। प्राय: जीएम फसलों के समर्थक कहते हैं कि वैज्ञानिकों का अधिक समर्थन जीएम फसलों को मिला है पर प्रो. भार्गव ने इस विषय पर समस्त अनुसंधान का आकलन करके स्पष्ट बता दिया कि अधिकतम निष्पक्ष वैज्ञानिकों ने जीएम फसलों का विरोध ही किया है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन वैज्ञानिकों ने समर्थन दिया है, उनमें से अनेक किसी न किसी स्तर पर जीएम बीज बेचने वाली कंपनियों या इस तरह के निहित स्वाथरे से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं, या प्रभावित रहे हैं। आज जब शक्तिशाली स्वाथरे द्वारा जीएम खाद्य फसलों को भारत में स्वीकृति दिलवाने के प्रयास अपने चरम पर हैं, इस समय बहुत जरूरी है कि इस विषय पर तथ्य और शोध आधारित चेतावनियों पर ध्यान दिया जाए।
शांति की कोशिशें
संपादकीय
आंतरिक जटिलताओं में फंसे मणिपुर में शांति के लिए किए जा रहे प्रयास जितने आवश्यक हैं, उतने ही सराहनीय भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर हैं और उनके क्रिया-कलाप से केंद्र और राज्य सरकार की गंभीरता का सहज ही एहसास हो जाता है। शांति बहाल करने के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं और आने वाले दिनों में भी सरकारों को हर मुमकिन फैसले के लिए तैयार रहना चाहिए। मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाल हो और स्थानीय समाजों में स्वाभाविक समन्वय फिर पैदा हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? परस्पर सहमति से जो फैसले लिए गए हैं, उन्हें तत्काल लागू करना चाहिए, ताकि जमीनी स्तर पर लोगों में संतोष और सुरक्षा भाव की वापसी हो। मणिपुर में 3 मई से ही कर्फ्यू की स्थिति है और इंटरनेट सेवा भी बाधित है, इससे लोगों को निस्संदेह परेशानी हो रही होगी, सामान्य सुविधाओं की बहाली बहुत जरूरी है। गौर करने की बात है कि शांति की तलाश में केंद्रीय गृह मंत्री दस से ज्यादा प्रतिनिधिमंडल से मिल चुके हैं। मैतेई और कूकी, दोनों ही समुदायों के प्रतिनिधिमंडल मिलकर अपनी बात रख चुके हैं। कुकी नेताओं ने हिंसा की सीबीआई जांच के लिए कहा है, तो यह भी स्वागतयोग्य है। हिंसा शुरू करने वाले और फैलाने वाले तत्वों की पहचान बहुत जरूरी है।
मणिपुर में कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करना, राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाना, जातीय संघर्ष में मारे गए लोगों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का फैसला कारगर हो सकता है। पीड़ितों के साथ सरकारों को खड़े हो जाना चाहिए और असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। राज्य के कई इलाकों में हिंसक तत्वों ने कानून-व्यवस्था का मखौल उड़ाया है। मणिपुर की छवि को भी झटका लगा है, अत: सुरक्षा एजेंसियों को अपने स्तर पर पूरी सतर्कता बरतते हुए हिंसक तत्वों पर लगाम कसनी चाहिए। निर्दोष और विस्थापित लोगों को जल्द से जल्द उनके घर लौटने के लिए प्रेरित किया जाए और सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री ने उचित ही अधिकारियों को राज्य में शांति भंग करने वाली गतिविधियों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर, विभिन्न समूहों से कम से कम 15 दिन शांति बनाए रखने की अपील की गई है। जाहिर है, मणिपुर में दूरदराज के इलाकों में ऐसे बहुत से लोग होंगे, जो फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे, उन तक राहत पहुंचाना केंद्र व राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है।
यह मणिपुर व पूर्वोत्तर की राजनीति के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। सभी राजनीतिक दलों को शांति प्रयासों में जुट जाना चाहिए। आदिवासी नेताओं, बुद्धिजीवियों और प्रमुख आदिवासी नागरिकों के साथ भी केंद्रीय गृह मंत्री की चर्चा का सार्थक परिणाम निकलना चाहिए। नए समय और आधुनिक होते समाज की रोशनी में स्थानीय लोगों को सकारात्मक योगदान देने के लिए सहर्ष आगे आना चाहिए। यह अच्छी बात है कि इतनी हिंसा के बावजूद स्थानीय स्तर पर सुरक्षा बलों ने संयम का परिचय दिया है। हिंसा फैलाने वालों को आतंकवादी नहीं समझा जा रहा है। हिंसा को संगठित हिंसा के बजाय जातीय हिंसा माना जा रहा है। वैसे, मौके का गलत फायदा उठाते हुए अलग राज्य की जो मांग उठी है, उस पर फिलहाल विचार करने से बचना चाहिए। अभी मणिपुर में गांव-गांव तक शांति की बहाली प्राथमिकता है।
Date:01-06-23
फिर विस्थापित विश्वास का मणिपुर
रामी निरंजन देसाई, ( विशेषज्ञ, पूर्वोत्तर मामले )

मणिपुर की जनजातियां इसके चरित्र को जटिल बनाती हैं। हम बेशक उनको कानूनी रूप से अनुसूचित जनजाति न बुलाएं, लेकिन वे खुद को अनुसूचित जनजाति ही मानती हैं। फिर, उनके अंदर भी कई उप-जनजातियां हैं, जिनमें खूब आपसी तनाव रहा है। 1997 में ही कुकी और उसकी उप-जनजाति पाइटी में जबर्दस्त हिंसा हुई थी। नगा भी यहां काफी हैं। फिर, म्यांमार से भी काफी संख्या में लोग भागकर यहां आए हैं, जिनको चिन कहा जाता है। इन सबके बीच संघर्ष तो है ही, जनजातियों के भीतर भी तनाव है। इससे मणिपुर अन्य राज्यों से अलग प्रकृति का हो जाता है।
जिस नजरिये से हम दूसरे राज्यों को देख सकते हैं, मणिपुर को नहीं देख सकते। यहां छोटे-मोटे तनाव होते रहे हैं, लेकिन पिछले पांच-छह साल में इसने जो उपलब्धि हासिल की है, वह उल्लेखनीय है। दशक-डेढ़ दशक पहले तक यहां शाम में चार बजे के बाद कफ्र्यू लग जाया करता था। ठहरने के लिए ढंग की जगह नहीं मिलती थी। परिवहन भी सुगम और सुरक्षित नहीं था। मगर अब यहां नए-नए होटल बन गए हैं। आना-जाना भी आसान हो गया है। नौजवान भी अब ज्यादा दिखने लगे हैं, क्योंकि वे पहले अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए बेंगलुरु, दिल्ली चले जाते थे। तमाम तरह के कारोबार यहां शुरू हो चुके हैं। तरक्की की इन इबारतों से जातीय तनाव की आग मानो चिनगारी में बदल गई थी। मगर अब ताजा हिंसा के बाद माना जा रहा है कि आपसी अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो जाएगी कि उसे पाट पाना काफी कठिन होगा। हाल-फिलहाल के दिनों में कुकी और मैतेई शायद ही एक-दूसरे पर भरोसा कर सकेंगे।
यह एक खतरनाक संकेत है। बेशक यहां अमन-चैन दिखने लगा था, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, और विकास के कई काम हुए हैं, लेकिन तमाम जनजातियों में आपस में प्रतिस्पद्र्धा भी है। और, दुर्भाग्य से इनमें से कई हथियारबंद समूह भी हैं। इस बार उन्होंने अपने हथियारों का प्रदर्शन किया है, चाहे वे लूटकर उन्होंने जुटाए हों या कहीं से उनको मिले हों। अतीत में यहां आलम यह था कि अलगाववादी गुटों की सक्रियता सब पर भारी पड़ती थी। इस कारण यहां के कई इलाके असुरक्षित माने जाते थे। राजधानी इंफाल को छोड़कर बाकी तमाम क्षेत्रों में विकास की रोशनी मानो पहुंच ही नहीं रही थी। नतीजतन, यहां पर्यटक भी नाममात्र के दिखते थे। मगर इन दिनों हालात काफी बदल चुके थे। मणिपुर को ‘न्यू रिफॉर्म्ड सेफ स्टेट’ यानी सुधार की नई राह पर आगे बढ़ता एक सुरक्षित राज्य माना जा रहा था। पिछले कुछ वर्षों में बनी यह तस्वीर मिनटों में ध्वस्त हो गई।
हमें यह समझना होगा कि गैर-कानूनी घुसपैठ यहां की सच्चाई है। म्यांमार में जब से सरकार बदली है, उसने पूर्वोत्तर को प्रभावित किया है। बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही है, जिसकी बिगड़ती सेहत पूर्वोत्तर को नुकसान पहुंचाती है। असल में, म्यांमार और भारत के सीमावर्ती इलाकों में बसी इन जनजातियों में पारिवारिक रिश्ता है। आतंकवाद के खिलाफ म्यांमार सरकार की कार्रवाई के बाद काफी संख्या में लोग सीमा पार से आए। वे मणिपुर ही नहीं, मिजोरम में भी बसे। वहां तो करीब 30 हजार शरणार्थियों को चिह्नित भी किया गया है। कोई यह पूछ सकता है कि जब मिजोरम में भी म्यांमार से प्रवासी आए, तो वहां ऐसा तनाव क्यों नहीं दिखता? असल में, मिजोरम में इनके समर्थन में आवाज उठी है। हालांकि, वहां भी जनसांख्यिकी में बदलाव का मसला आ सकता है, जिसका गवाह मणिपुर बना है। यहां के चुराचांदपुर इलाके की आबादी करीब दो दशक पहले तक 60 हजार थी, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग छह लाख हो गई है। फिर, इस तरह का प्रवासन किसी खास समुदाय के पक्ष में होता है। चूंकि सीमा पार से आने वाले ज्यादातर लोग स्वजातीय कुकी बहुल इलाकों में बसते गए, इसलिए मैतेई खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। ऐसे प्रवासन अलगाववादियों के लिए भी खाद-पानी का काम करते हैं। नगा विद्रोह के दौरान हमने देखा ही था कि किस तरह से विद्रोहियों को चीन का साथ मिला। त्रिपुरा में ही विद्रोही गुटों को बांग्लादेश में प्रशिक्षण हासिल हुआ था।
आखिर इसका समाधान क्या है? जब मौजूदा तनाव शुरू हुआ था, तब कहा गया था कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मैतेई को अनुसूचित जनजाति बनाने संबंधी सिफारिश करने के लिए ‘निर्देशित’ किया है, जबकि असलियत में यह प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि इस मांग को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हवाले किया जाना था। इतना ही नहीं, कुकी अब जंगली क्षेत्र में छठी अनुसूची लागू करने की मांग करने लगे हैं, जिससे यहां के स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रों में स्थानीय परिषद को न्यायिक और दूसरी विधायी शक्तियां मिल जाएंगी। उल्लेखनीय है कि ऐसी हर परिषद को समान अधिकार नहीं दिए जाते। किसी-किसी को तो तमाम शक्तियों से वंचित भी रखा जाता है। हालांकि, ये तमाम अधिकार तभी मिलते हैं, जब समुदाय विशेष अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर दिखता है।
विरोध जताना देश के नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है, और कुकी यदि यहीं तक सीमित रहते, तो कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकते थे। मगर अब बात हिंसा और हथियार तक पहुंच गई है। चूंकि यहां की जनजातियां सिर्फ अलगाववादी गुट नहीं हैं, इसलिए इस मसले के समाधान में सिविल सोसाइटी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। सत्ता-प्रतिष्ठान निस्संदेह जरूरी होने पर सख्ती दिखाए, लेकिन अमन का रास्ता मिल-बैठकर बातचीत करने से ही निकलेगा। यहां के समुदाय अपने हितों के लिए अपनों की जान-माल और सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकते। उनका यह रुख किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं कहा जाएगा।
