
लोकतंत्र की महत्ता केवल चुनावों में नहीं है।
Date:12-06-18 To Download Click Here.
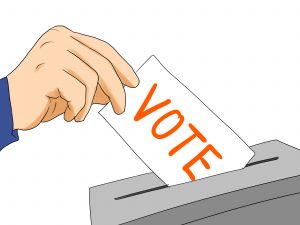
अब सवाल यह है कि प्रजातंत्र चुनाव सम्पन्न कराने के अलावा और क्या हो सकता है? इसके लिए हमें सबसे पहले मतदान के महत्व को समझना होगा। किसी एक व्यक्ति को वोट देकर आखिर हम क्या सिद्ध करते हैं? आज जब मतदान एक व्यवसाय बन चुका है, ऐसे में उसकी क्या महत्ता है? वास्तव में वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है?
मतदान का महत्व इसलिए नहीं है कि उसके द्वारा विकल्प मिल जाते हैं बल्कि इसलिए है कि उसके द्वारा हम किसी प्रतिनिधि को शक्ति प्रदान करके उसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेह बना रहे हैं। चुनाव तो शक्तिसंपन्न प्रतिनिधियों को नियंत्रित करने का साधन है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी चुनाव अपने ही दायरे में खत्म हो जाता है। इस प्रकार, लोकतंत्र का सार वास्तव में चुनने की स्वतंत्रता में नहीं है। बल्कि वह मुख्य रूप से निर्वाचित शक्ति से जुड़ा है। प्रजातंत्र को विकल्प चुनने मात्र से जोड़ देना और यह दावा करना कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था प्रजातंत्र का प्रतिबिम्ब है, बहुत ही गलत है। भारत में ऐसी विचारधारा का परिणाम यह हो रहा है कि निर्वाचित शक्ति ही अप्रजातांत्रिक होती जा रही है।
ऐसी स्थिति में चुनावों की सार्थकता क्या है? हम किसी को क्यों चुन रहे हैं? चुनाव की सार्थकता इसलिए है कि यह समाज के संसाधनों के समान वितरण की मूल धारणा को लेकर चलता है। इसे इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि हम किसी समाज के समान बाशिंदे हैं, और इसके प्रशासन और सम्पत्ति पर हमारा समान अधिकार है। व्यवहार में, सार्वजनिक सम्पत्ति या संसाधनों पर एक निर्धन का भी उतना ही अधिकार है, जितना कि एक धनी का। किसी व्यक्ति का चुनाव करके या उसे प्रतिनिधि बनाकर हम उसे इसी सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा का भार सौंपते हैं। इस प्रतिनिधि द्वारा इस भारत के निर्वहन के तरीके में ही प्रजातंत्र का असल मर्म छिपा हुआ है।
इसे न्यायधारिता या ट्रस्टीशिप भी कहा जा सकता है। गांधीजी ने भी इसकी जबर्दस्त वकालत की थी। निर्वाचित प्रतिनिधि तो हमारे एवज में महज एक ट्रस्टी है। इस ट्रस्टी का यह प्रधान कर्त्तव्य है कि वह उस सम्पत्ति की रक्षा करे, जिसके लिए उसे ट्रस्टी बनाया गया है। प्रजातंत्र का यही एक निहितार्थ है। आज यही अर्थ नष्ट होता जा रहा है। सुशासन का विचार भी इसी से जुड़ा हुआ है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे अपने इस कार्य को सुचारू ढंग से सम्पन्न करें। इसका इतना सा ही अर्थ है कि वे हमारे एवज में ऐसे निर्णय लेकर उन्हें क्रियान्वित करें, जिनसे कि सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा हो सके। इसके स्थान पर वे हमारे हिस्से को भी अपनी व्यक्तिगत विकास में लगाने लगते हैं।
राजनीति में प्रजातंत्र की शुद्ध आत्मा की कमी का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है। समाज में कुछ ही ऐसे संस्थान हैं, जो प्रजातंत्र के शुद्ध विचार को आत्मसात करके चलते हैं। इस क्षेत्र में कुछ निजी संस्थान हैं, जो प्रजातंत्र की आत्मा की रक्षा का दिखावा कर लेते हैं। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, ये निजी संस्थान, सार्वजनिक सम्पत्ति के एक हिस्से की ट्रस्टीशिप में साझेदार हैं। हम निःसंकोच इस ‘निजी’ से कुछ नैतिक आचार-व्यवहार की अपेक्षा रख सकते हैं, क्योंकि आखिर तो इन्हें भी अपने अस्तित्व के लिए एक दृढ़ सार्वजनिक आधार चाहिए होता है। इन संस्थानों से भी केवल विकल्प के चुनाव की पूर्ति के अलावा कुछ अधिक अपेक्षित होता है। यह तभी हो सकता है, जब शक्ति या सत्ता का लोकतांत्रीकरण संभव हो। वर्तमान में, हम सब यह जानते हैं कि छोटे-छोटे संस्थानों में भी शक्ति का प्रजातांत्रिक बंटवारा कठिन होता जा रहा है। चाहे सरकार हो या अन्य कोई संस्थान, जब तक सत्ता सम्पन्न व्यक्ति के अंदर एक ट्रस्टी होने का भाव रहेगा, तब तक प्रजातंत्र की कुछ रक्षा होती रहेगी।
मतदाता तो केवल उस समय तक राजनीतिक प्रक्रिया का एक अंग होता है, जब तक वह मतदान करता है। इसके पश्चात् लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वह पृथक हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया को सही मायने में लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता। लोगों में राजनीति से अलगाव की भावना का जन्म हो रहा है। इस राजनीतिक उदासीनता से ही सांस्कृतिक निष्क्रियता का जन्म हो रहा है। परिणामस्वरूप दक्षिणपंथी ऊभर रहे हैं। अगर हमें वर्तमान में आ रही समस्याओं से मुक्ति चाहिए, तो हमारी राजनीतिक प्रक्रिया को सही मायने में लोकतांत्रिक और समावेशी बनाना होगा। यही आम आदमी की मांग है।
‘द हिन्दू’ में प्रकाशित सुंदर सरूकई के लेख पर आधारित। 22 मई, 2018
