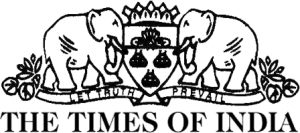24-11-2016 (Important News Clippings)
To Download Click Here
Welcome demise
Donald Trump’s vow to pull the US out of TPP is good for India
US President-elect Donald Trump recently took to social media to outline his policy plans for the first 100 days in the White House. And the highlight of Trump’s two-and-a-half-minute YouTube video was his vow to pull out of the Trans-Pacific Partnership (TPP) on his first day in office. Touted as a marquee trade deal between 12 Pacific countries – including the US, Japan and Canada – TPP was the outgoing Obama administration’s lynchpin in Washington’s pivot to Asia. Strategically, it signalled American intent in writing the rules of the road for commerce in Asia while keeping China out.
But an American pullout means the end of the road for TPP. From the Indian perspective, this is a good thing. TPP’s excessive emphasis on intellectual property and other nontariff barriers discomfited India. While India kept out, had the trade deal been operationalised other Asian countries would have scored over India in terms of market access to the US and Japan. In contrast, the Regional Comprehensive Economic Partnership which includes India, Japan, China and Southeast Asian countries is less demanding of New Delhi. But this trade pact is also beset by concerns about China’s export muscle.Against this backdrop, the WTO process is best suited for India even though its consensus-based decision making isn’t fast. And TPP’s demise does create some uncertainties. If a President Trump actually pulls America out of Asia it would be worrying for India. The US has an important role to play in Asia. Its support is needed to maintain the strength of regional platforms such as the India-Japan-US trilateral and the East Asia Summit. Hopefully, Trump will realise when in office that the US does have a strong interest in Asia.
Don’t underestimate e-banking capacity

Thanks to the National Payments Corporation of India’s (NPCI) National Unified USSD Platform, anyone with a bank account and an active phone linked to the bank account can transfer money to another bank account, using what NPCI calls Immediate Payment Service, or IMPS. USSD is a protocol used by all GSM phones, not just smartphones, to establish a two-way data link between the phone and a designated set of computers. The recently launched Unified Payments Interface (UPI) calls for a smartphone with an internet connection, still a rarity in rural India. With minimal effort, anyone with a phone can get a mobile money identifier and a mobile personal identification number. People have to be trained to get these two numbers from the bank and to use them. In urban areas, the UPI can be pushed but in rural areas, IMPS must be popularised.
The RBI recently increased the limit for the money that e-wallets can spend in a month, from Rs 10,000 to Rs 20,000. But for a merchant, the amount he can receive is a measly Rs 50,000 a month from e-wallets. This makes no sense whatsoever. There is no reason for any limit at all, as there is complete traceability for the amounts the merchant receives into his e-wallet. This show of excessive caution will prevent people from using prepaid payment instruments on the scale they potentially can. It is self-defeating and should be removed.
मतदाता के अधिकारों की दिशा में एक फैसला
देश की अदालतों ने समय-समय पर मतदाताओं के पक्ष में फैसले दिए हैं। इससे मतदाताओं के अधिकारों में न केवल स्पष्टता आई है, वरन इजाफा भी हुआ है, साथ ही लोगों का शिक्षण हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाता को यह मौलिक अधिकार है कि वह प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता जाने।
नौकरशाही में भ्रष्टाचार पर करें कड़ा प्रहार
अगर प्रधानमंत्री अपने अभियान में पूरी तरह सफल होना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर लगानी होगी लगाम। बता रहे हैं टीसीए श्रीनिवास राघवन
सरकार के 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले से मची अफरातफरी ने पिछले दो हफ्ते से कालेधन के मुद्दे पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। लेकिन इस बहस में बड़ी हिस्सेदारी आंख पर पट्टी बांधे हुए उन लोगों की है जो हाथी के अलग-अलग अंगों को छूकर उसे परिभाषित करने में लगे रहते हैं और आखिर तक उनमें उस जानवर के स्वरूप को लेकर सहमति नहीं बन पाती है।
पूरी चर्चा के दौरान लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में केवल दो प्रकार का कालाधन ही होता है। काले धन का पहला रूप ईमानदार लोगों की छिपी हुई आय के तौर पर इक_ïा होता है जबकि दूसरा रूप अपराधियों की जानबूझकर छिपाई हुई आय की शक्ल में होता है।
लेकिन भारत में तीसरे तरह का काला धन भी मौजूद है और वह अलग प्रकृति का ही है। इसमें पहले दोनों तरह के लोग और दोनों तरह की आय का बड़ा हिस्सा शामिल है। यह इस सार्वभौम देश की सेवा के लिए नियुक्त लोगों की आय के रूप में है। ये लोग दूसरों से उस काम के लिए उगाही करते हैं जिन्हें करने के लिए उनकी नियुक्ति की गई होती है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर सरकारी कर्मचारी एक-दूसरे का भी भरपूर शोषण करते हैं। इस गोरखधंधे में कोई भी बच नहीं पाता है।
जब ईमानदार लोग अपनी आय का कुछ हिस्सा छिपाकर रखते हैं तो उससे किसी अन्य को कोई परेशानी नहीं होती है। यहां तक कि अपराधी भी अपने गलत कार्यों से धन अर्जित करते हैं तो उसमें केवल पीडि़त व्यक्ति ही परेशान होता है। लेकिन भारत में इस तीसरे तरह के काले धन के लिए सरकारी कर्मचारी हर किसी को अपनी चपेट में लेते हैं। वे एक तरह से कैंसर की तरह हैं। वे किसी को भी नहीं बख्शते हैं, यहां तक कि अंतिम संस्कार के लिए अपने प्रियजनों के शव लेकर जाने वाले लोगों से भी ये कर्मचारी सूखी लकड़ी के नाम पर रिश्वत की मांग करते हैं। उनके ऐसे ही लोगों के कारनामों के चलते शायद जनता का एक बड़ा हिस्सा बड़े नोटों को बंद करने के कदम का समर्थन कर रहा है।
तीन रंग
नोटबंदी के फैसले की जो आलोचना हो रही है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोग काले धन के इन तीनों समूहों के बारे में एक साथ सोचने लगे हैं। फैसले के चलते आम जनता को हो रही परेशानी को समझा जा सकता है लेकिन काले धन के प्रवाह की समस्या के समाधान में इससे कोई ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली है। काले धन के भंडारण पर हमला बोलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले धन के प्रवाह पर सीधी चोट करनी होगी। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री को यह समझना होगा कि दोनों तरह के कामों के लिए उन्हें अलग रवैया अपनाने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा।इस दिशा में कदम उठाते ही तमाम नेता उठ खड़े होंगे और लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए विरोध तेज कर देंगे। आखिर सच तो यह है कि काले धन का सबसे ज्यादा फायदा तो नेताओं को ही होता है।
कानून का मौजूदा स्वरूप तो ऐसा है कि ईमानदारी से कमाने वाले लोग ही उसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर तमाम तरह के करों से बचने के लिए ये लोग अपनी आय का कुछ हिस्सा छिपाकर रखते हैं तो उन पर सरकारी विभाग पुरजोर ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक अपराधियों के कालेधन का सवाल है तो सरकार उनके प्रति उतना बलपूर्वक कदम नहीं उठाती है। इनमें से बहुतों को ऊपर से संरक्षण मिला होता है और कुछ तो चुनाव लड़कर सांसद-विधायक बन जाते हैं। अनैतिक तरीके से करोड़ों कमाने वाले कारोबारियों पर नकेल कसी जाती है तो वे विदेश भाग जाते हैं।ईमानदार छवि वाले प्रधानमंत्री मोदी अगर चाहते हैं कि करारोपण से बचने के चक्कर में पैदा होने वाले कालेधन पर रोक लगाई जाए तो उन्हें सरकार की जेब भरने वाले तरीकों पर निश्चित तौर पर गौर करना होगा। आयकर, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), स्टांप शुल्क और निगम कर जैसे शुल्कों को कम करना होगा जिससे भ्रष्टाचार में भी काफी गिरावट आएगी। जीएसटी दर के करीब 18 फीसदी होने पर आयकर की दरों को 15 और 25 फीसदी के स्तर पर लाया जाना चाहिए। आयकर की दरों में कटौती के फैसले से अधिक संख्या में लोग इसके दायरे में आएंगे, जैसा कि 1997 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने किया था।
खुद ही करनी होगी पहल
भारत में सरकार काले धन को लेकर काफी लचीला रवैया अपनाती रही है। संप्रभु देश के विभिन्न अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में इसे देखा जा सकता है। किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के आदेश सरकार विरले ही देती है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हटाने की जटिल प्रणाली से भी उन्हें काफी हद तक संरक्षण मिल जाता है। कुछ उच्च पदों के लिए तो महाभियोग का प्रावधान किया गया है।यही वजह है कि अगर प्रधानमंत्री काले धन के खिलाफ मुहिम में पूरी तरह सफल होना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले इस तबके पर ही निशाना साधना होगा। इन लोगों को आम तौर पर ईमानदारी से आजीविका कमाने वाले लोगों के शोषण की अब और इजाजत नहीं दी जा सकती है। इनकी नाइंसाफी की इंतेहा हो चुकी है। आखिर हम काफी हद तक बेईमान अधिकारियों से कैसे यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वे दूसरों को कानून के हिसाब से चलने के लिए मजबूर कर सकेंगे।मोदी कई बार अपने भाषणों में यह जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें सरकार के भीतर मौजूद भ्रष्टाचार का अहसास है। लेकिन इस दिशा में अब तक उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ऐसा लगता है कि वह आम करदाताओं के पैसे से वेतन लेने वाले कर्मचारियों पर सख्त कदम उठाने से भयभीत हैं। अगर साफ-साफ कहें तो सरकार के मौन समर्थन से ही ये कर्मचारी आम लोगों का खून चूसते हैं और काले धन का भंडार खड़ा कर लेते हैं। मोदी को इस समस्या का ही हल निकालना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो विमुद्रीकरण का फैसला उनके लिए बेहद महंगी चाल साबित होगी जिसमें उन्हें शिकस्त भी खानी पड़ेगी।इसका एक और फायदा यह होगा कि चिदंबरम की बोलती बंद हो जाएगी। आखिर चिदंबरम ने ही तो टैक्स अधिकारियों को वसूले गए कर में से एक हिस्सा देने की पेशकश कर वसूली को एक तरह से कानूनी बना दिया था। उस कदम से भारी भरकम टैक्स का नोटिस भेजने और बाद में समायोजित कर देने की प्रवृत्ति की शुरुआत हुई थी
टीसीए श्रीनिवास राघव
Date: 24-11-16
नियमन की प्रक्रिया को ज्यादा गंभीर बना देते हैं विनियामक
टाटा समूह के मुंबई स्थित मुख्यालय बॉम्बे हाउस में मची उथलपुथल के अलावा एक और वाणिज्यिक गतिविधि ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। वह है पूंजी बाजार में स्वतंत्र अभिव्यक्ति को सीमित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से जारी परामर्श पत्र। इसमें यह प्रस्ताव रखा गया है कि केवल निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकृत व्यक्ति या संस्था ही एसएमएस, ई-मेल या फोन के माध्यम से लोगों को निवेश के बारे में सुझाव दे सकता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति पंजीकृत निवेश सलाहकार नहीं है तो उसे व्हाट्सऐप, चैटऑन, वीचैट, ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया माध्यमों के जरिये भी निवेश सलाह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस पाबंदी से केवल खास तरह के लोगों को ही छूट देने की बात कही गई है। सेबी का मानना है कि प्रतिभूति बाजार के बारे में खुलकर राय रखने से धोखाधड़ी की आशंका बढ़ जाती है और इन नियमों से उन्हें रोका जा सकता है।
सेबी का यह परामर्श पत्र कई दिन पहले सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी किया गया है लेकिन आलोचकों का ध्यान इसने कुछ दिन पहले ही खींचा है। देखते ही देखते प्रस्तावित नियमों की आलोचना काफी मुखर हो चुकी है। हालांकि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता में बैठे लोगों के उठाए किसी भी कदम का समर्थन करने को तैयार हैं। उनका यह मानना है कि प्राधिकार में बैठे लोगों को शायद दैवीय ज्ञान मिला होता है। वे निवेशकों के हितों की सुरक्षा के नाम पर इन प्रस्तावों को उत्कृष्ट आदर्श बताते हुए पूरा समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सेबी का यह कदम भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है?
हमारे संविधान में सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि इस तरह की स्वतंत्रता पर तर्कसंगत पाबंदी लगाई जा सकती है। इस हिसाब से सेबी की तरफ से सुझाई गई पाबंदियों को तभी संवैधानिक बताया जा सकता है जब वे तर्कसंगत हों। आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में कोई टिप्पणीकार कहता है कि अमुक कंपनी के अबूझ फैसलों के चलते उसके शेयरों में गिरावट आ सकती है। या फिर कोई विश्लेषक यह मान लेता है कि ऊंचा कद रखने वाले कुछ लोगों का फैसला होने से अमुक कंपनी के शेयर ऊपर ही जाएंगे। अगर उसने सेबी के तहत निवेश सलाहकार के रूप में अपना पंजीकरण नहीं करा रखा है तो सेबी के प्रस्तावित कानून में ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सऐप पर इस तरह की राय व्यक्त करना गैरकानूनी हो जाएगा।
अपनी राय रखने वाला हरेक शख्स अब निवेश सलाह नहीं दे सकेगा। उसे कानूनी वैधता के लिए निवेश सलाहकार के रूप में अपना पंजीकरण कराना होगा। इसका मतलब है कि आर्थिक मामलों पर अपनी राय रखने वालों को पूंजी बाजार नियामक के पास अपना पंजीकरण कराना होगा, भले ही यह उनका मूल व्यवसाय न हो। इससे भी बुरी बात यह है कि अगर कोई निवेश के बारे में अपनी राय रख देता है तो वह उसकी सत्यता और सटीकता से परे प्रतिभूति धोखाधड़ी का आरोपी बन जाएगा। इसके लिए उस पर 25 करोड़ रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है या 10 साल तक का कारावास दिया जा सकता है या फिर सेबी के पास पंजीकरण होने तक अपना मुंह बंद रखने की हिदायत देकर उसे छोड़ा जा सकता है। इस बदलाव का पूंजी बाजार में विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी पर ‘डरावना असरÓ पड़ेगा। यह एक ऐसा कदम होगा जिसे शायद ही तार्किक कहा जा सकता है।
दरअसल हम भारतीय हर तरह के मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। भले ही वह अमेरिका में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव। ऐसे में आप एक ऐसे कानून की कल्पना कीजिए जो आपको मायावती के जीतने या यादव खानदान के एक धड़े की जीत के बारे में चर्चा करने के लिए अपराधी ठहरा सकता है, अगर आप पंजीकृत चुनाव विश्लेषक नहीं हैं या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं हैं।
हालांकि प्रतिभूति बाजार में स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर रोक की मांग करने वाले लोग यह तर्क दे सकते हैं कि वित्तीय बाजार और चुनाव में काफी हद तक असमानता है। आखिर पूंजी बाजार में लोग किसी की राय से प्रभावित होने पर बड़ी रकम गंवा सकते हैं जबकि दूसरे मामले में लोगों को एक खराब सरकार ही तो मिलेगी। इस पर मेरा यह कहना है कि खराब सरकार का मिलना किसी नागरिक के लिए अधिक बुरा हो सकता है क्योंकि पूंजी बाजार में गंवाए पैसे को तो वह फिर से कमा सकता है। दूसरा, यह पता लगा पाना खासा मुश्किल है कि कौन सी राय निष्पक्ष है और कौन सी राय किसी खास मकसद से प्रेरित होकर रखी गई है? किसी नियामक संस्था के पास पंजीकरण करा लेने से हालात तो नहीं बदल जाएंगे। चुनाव संबंधी कानूनी मामलों में भी अदालत यह विचार करती है कि किसी उम्मीदवार ने गलत तौर-तरीका तो नहीं अपनाया था। इसी तरह सेबी भी शेयरों के बारे में लगाए जाने वाले अनुमानों के पीछे के मकसद की पड़ताल करता है। दरअसल नियामकीय संस्थाओं में बैठे लोग अपने कदमों को सही ठहराने के लिए अपने कार्य को खूब बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं, भले ही वह कितना भी दोषपूर्ण क्यों न हो? निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए जिस तरह के आदर्श रखे
गए हैं, उनका विस्तार तो खानपान, बिजली आपूर्ति, दवाओं से लेकर टैक्सी सेवा तक होना चाहिए। ये आदर्श काफी ऊंचे तो हो सकते हैं लेकिन उन्हें हासिल करने के तरीके तो व्यावहारिक और संवैधानिक दायरे में ही होने चाहिए।
सोमशेखर सुंदरेशन (लेखक स्वतंत्र विधिक परामर्शदाता हैं।)
No complacency on Zika
The World Health Organisation has declared that the Zika virus no longer constitutes a public health emergency of international concern. This brings to an end the heightened global focus on the virus that has caused about 2,300 confirmed cases of microcephaly (a birth defect manifesting in a smaller head size) since May 2015. The WHO had declared the Zika virus a public health emergency on February 1, considering the high number of neurological disorders reported in Brazil and a similar cluster in French Polynesia in 2014. Among the reasons cited were the unknown causal link between the virus and microcephaly and neurological complications, the possibility of its global spread, lack of vaccines and diagnostic tools, and the lack of immunity to the virus in newly affected countries. The link between Zika and microcephaly was established in May, the hunt for a potent vaccine and reliable diagnostic tool has begun, and scientists have been able to find the routes of transmission. However, the global risk assessment has not changed. The spread of Zika to 67 countries and territories is a grim reminder of the lack of immunity against the virus and the abundance of mosquito vectors. A dozen countries have reported local transmission.
Despite the link between the Zika virus infection and microcephaly being well established, the entire spectrum of challenges posed by the disease is not known. The WHO Emergency Committee has called for sustained research and dedicated resources to address the long-term challenges posed by babies born with microcephaly, but signalling the end of the global emergency may lead to lowering of the global alert. There should be no setback to funding, the global search for effective vaccines and diagnostic tests, and creating awareness about the risk of sexual transmission. For instance, it is not clear why more babies were born with microcephaly in northeast Brazil compared to the rest of the country or why the country had a higher caseload than others. This information is crucial to understanding the link between Zika infection and microcephaly, and thereby to containing incidence where the mosquito vector is predominant. Medical journals should continue to provide free and immediate access to papers on the Zika virus, which played a crucial role in information-sharing. The WHO has said it is “not downgrading the importance of Zika” and that its “response is here to stay”. It now needs to ensure that vigilance remains high despite the decline in incidence.
Death of a pact
Trump’s announcement on the Trans-Pacific Partnership goes to the heart of the new global order.
In April, US President Barack Obama warned Asia-Pacific leaders: “If we don’t write the rules, China will write the rules”. That prophecy, full of potentially grim consequences for India is now upon us. President-elect Donald Trump declared on Monday that he intends to withdraw from the Trans-Pacific Partnership trade deal on his first day in office, calling it “a potential disaster for our country”. Instead, Trump says, he intends to “negotiate fair bilateral trade deals that bring jobs and industry back”. The declaration is, in fact, less important than it sounds. President Obama gave up his efforts to have the 12-nation trade deal ratified by the US Congress a week ago, recognising, perhaps, that it had no traction: Even Trump’s rival, Hillary Clinton, had said she would veto the deal.
Japanese Prime Minister Shinzo Abe, the first foreign leader to meet Trump, is believed to have used their 90-minute meeting to drive home the importance of the Trans Pacific Partnership — but the statement from America’s President-elect showed his efforts were in vain. The consequences of this action, however, go far beyond a trade agreement, to the very heart of the global order — an order on which India’s rise is predicated.
Last week, China’s President, Xi Jinping, showed willingness to step in where the US has stepped back, declaring at the Asia Pacific Economic Cooperation group’s meeting in Lima that “openness is vital for the prosperity of the Asia-Pacific”. China has been pushing the Regional Comprehensive Economic Partnership — an arrangement that does not include the US, just as the Trans Pacific Partnership excluded China.
Even nation-states sceptical of a China-led world order are willing to join up. “We like the US being in the region”, New Zealand Prime Minister John Key said at the Lima summit, “but if the US is not there, that void needs to be filled, and it will be filled by China”.
The fact is, China, the largest source of growth in the global economy, is the main trading partner of 120 of 196 nations. Trump’s plans to charge nations for upholding the global order — and protecting common assets like trade routes, energy security or the environment — make US claims to shape global norms even more tenuous. It is far from clear, though, whether China is in a position to shape the new norms, let alone enforce them. President-elect Trump’s actions could well signal the coming of a new global anarchy.
Date: 23-11-16
Not so Pacific now
The Asia-Pacific is changing. With Donald Trump withdrawing US influence and China increasing its power, India must re-strategise

Strategically, Asia has emerged as a nerve centre. Asia’s defence spending is now larger than Europe’s. Reports indicate that in 2014, military spending in Asia increased by five per cent, reaching around $439 billion in total, compared to Europe’s spending, which grew by 0.6 per cent, reaching around $386 billion in total.
The region, hitherto called Asia-Pacific, should now be renamed Indo-Pacific. Asia-Pacific came into vogue half a century ago when Japan rose to prominence. Today, the entire Indian Ocean region has grown into an economic juggernaut. The global power axis has shifted from the Pacific-Atlantic to this region. Half of the world’s submarines will roam the Indo-Pacific region in the next two decades — at least half the world’s advanced combat aircraft, armed with extended range missiles, supported by sophisticated information networks, will also be operated by countries here.
Longer-range precision-guided missiles, including ship-based missiles, advanced intelligence, surveillance systems, autonomous systems like unmanned combat vehicles, in operation in the sub-surface, surface and air — this will be the region’s future. An Australian study indicates: “Over the next two decades, other technological advances such as quantum computing, hypersonics, energy weapons and unmanned systems are likely to lead to the introduction of new weapons into our region. By 2035, more countries in our region will have access to ballistic missile technology… The next 20 years will see the expansion of space-based and space-enabled capabilities, including military capabilities.”
This great power brings greater responsibility on nations in the region. Countries like India face greater challenges and need to equip themselves for these. The Asia-Pacific region has been a playground of big power politics in the last few decades. The US has vast interests, assets and allies here. President Obama talked of the “Asian pivot” and “rebalancing” in the region. He took interest in forging a new regional alliance, called the Trans-Pacific Partnership (TPP).
But the situation is changing fast. US President-elect Donald Trump doesn’t seem to share President Obama’s interest or enthusiasm in these matters. He described TPP as “catastrophic” and vowed to dismantle it. Together, 12 countries had drafted the 3,000-page TPP agreement in February 2016 at Auckland, New Zealand. But it is unlikely to see the light of day in America as the Republican-dominated US Congress has refused to ratify Obama’s brainchild. In the words of the commander of the US Pacific Command, Admiral Harry Harris, “TPP is more or less dead.”
After the TPP fiasco, it is likely that the role of the US in the region is going to significantly diminish under Trump. Although Trump talked tough about China, that was largely in the context of the US economy and jobs. In fact, an international magazine reported, quoting a senior scholar in China, that the Chinese government was happy about Trump’s election because the leadership there thinks that now, “America would no longer be at their backs.”
With America’s role diminishing in the region, China will emerge as much more powerful now. It has already built several new regional alliances through projects like One Belt One Road (OBOR), Maritime Silk Road, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and Shanghai Cooperation Organisation (SCO). President Xi Jinping, who has now acquired the status of “Core Leader”, is pushing hard for another regional alliance called the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). It was originally conceived as China’s response to Obama’s TPP. TPP is dead — but RCEP is racing ahead. India is not a partner in either of the groupings thus far. But it will be forced to take a view on RCEP in view of its status and interests in the region.
Significantly, the rule-based global order is also coming under tremendous pressure in the region with countries violating established norms with impunity. Multilateral institutions seem utterly helpless while countries continue with activities detrimental to regional peace. North Korea’s nuclear programme, developments in the South China Sea and increasing cyber violations are examples of this trend.
Under the circumstances, India can no longer remain a reticent nation in regional and global politics. In the last couple of years, India has given some indications that it has arrived. It started showing more interest in the UN’s affairs. It played a crucial role at the Paris Climate Summit and became increasingly assertive about its rights in the NSG, UN Security Council, etc.
PM Modi has set the tone for this in 2014 during his first visit to the US, “India is already assuming her responsibilities in securing the Indian Ocean region. A strong India-US partnership can anchor peace, prosperity and stability from Asia to Africa and from the Indian Ocean to the Pacific. It can also help ensure security of the sea-links of commerce and freedom of navigation on seas.”The new century now brings India face to face with these new realities. We need to face them because there is no other option.The writer is national general secretary, BJP, and director, India Foundation. This is an edited version of his speech delivered at the Halifax International Security Forum (November 18-20, 2016), Halifax, Canada
Date: 23-11-16
An ill-judged conflict
Populism based on opposition between an elected legislature and the judiciary does not bode well for a democracy based on rule of law.

The challenge it — and, the judiciary at large — faces today may not look as enormous compared to what it faced in the 1970s. But a peril of this magnitude has not manifested itself since the 1970s and tensions between the judges and the government have never been so intense for such a long period.
The issue responsible for these tensions — vacancies in courts — is not new. I highlighted them in detail in an article last year (‘Holes in the government,’ The Indian Express June 4, 2015). But the holes have become larger. In May 2015, vacancies represented 35.9 per cent of the total approved strength of the judges in the Supreme Court and High Courts — 366 out of 1,017. By November 2016, the vacancies had increased by almost seven percentage points — 42.7 per cent (461 out of 1,079). Some states are more affected than the others. These include strife-prone states such as Chhattisgarh where 50 per cent (11 out of 22) of the judges posts lie vacant. What kind of justice can a state administer when half of the judges’ posts have not been filled up? Regions which are more calm have also been penalised. These include Andhra Pradesh (60.6 per cent vacancies), Karnataka (59 per cent), Uttar Pradesh (51.25 per cent) and Assam (45.8 per cent).
True, some states with a very high vacancy rate have a smaller backlog of cases. Tamil Nadu, where the vacancy rate was very high till recently (49 per cent this summer), is a case in point. While it has a very low judge-population ratio (14 judges per million population in contrast with states like Delhi which has 47 judges per million population or Gujarat which has 32 judges per million population), it also has a low pendency rate. But inevitably, there is a correlation between the effectiveness of the judiciary and the number of judges. That is why Supreme Court judges argue that the number of pending cases will never diminish if the number of vacancies keeps increasing. Chief Justice T.S. Thakur declared in May that 70,000 more judges were required to clear the pending cases.
Why doesn’t Narendra Modi’s election promise, “Minimum government, maximum governance”, hold good in the domain of law? There is an obvious explanation: It lies in the tussle over the procedure for appointing judges, which goes back to 2014. After taking over power, the Modi government introduced a bill in Parliament, which was intended to put an end to the collegium system (in a nutshell, this involved judges appointing judges) and to create a National Judicial Appointments Commission (NJAC). The commission would have comprised the Chief Justice of India (CJI), two other senior judges of the Supreme Court, the law minister and two other “eminent” persons appointed by a committee consisting of the prime minister, the CJI and the leader of the opposition. The NJAC would have been responsible for the appointment and transfer of judges to the higher judiciary. The Commission was established in August 2014 through the 99th amendment to the Constitution of India. The Bill was passed and approved by more than 16 states. But in October 2015 the Supreme Court decided to strike down this reform and to revive the collegium system in the name of the independence of the judiciary.
However, the Modi government did not resign itself to the status quo. It drafted a Memorandum of Procedure (MoP) that was supposed to improve the decision-making process regarding the appointment of judges. This MoP was sent to the Supreme Court in March. In May, the CJI returned it with the views of the collegium, which rejected at least two clauses: The need for judges to write their reasons for promoting (or rejecting) X or Y that the government had introduced for the sake of transparency and the possibility for the government to reject any name recommended by the collegium on grounds of national security.
Because of these bones of contention, for months, no real collaborative work has been possible between the executive and the judicial wings of the Indian state. They merely agreed to appoint retired judges in high courts to tackle pendency — and that too in early November, after months of a difficult dialogue. In between, a bench of the Supreme Court had told Attorney General Mukul Rohatgi that the court would not allow the judicial “institution to be decimated by the inaction, inefficiency or unwillingness of the executive”. Can decimation be a strategy for weakening a judiciary which has shown its independence lately by reinstating governments in Arunachal Pradesh and Uttarakhand in response to President’s rule? Such an interpretation is supported by the recent decision of the Union government to return 43 of the 77 names recommended by the collegium for appointment of judges in high courts, a first since, till then, the primacy of the CJI had prevailed in this matter.
This move reflects the government’s perception of the role of the judiciary, that has been well articulated by Arun Jaitley. After the rejection of the NJAC by the Supreme Court, he said that “democracy can’t be the tyranny of the unelected” and also: “There is no principle in democracy anywhere in the world that institutions of democracy are to be saved from the elected”. Emphasising that the popular vote was the keystone of democracy, he also declared that “Just as independence of the judiciary is part of basic structure [of the Constitution], the primacy of the legislature in policymaking is also part of basic structure.”. On the day the Supreme Court made it possible for Harish Rawat to return as chief minister of Uttarakhand, Arun Jaitley declared in the Rajya Sabha that Parliament should make its own decision about the Goods and Services Tax because “With the manner in which encroachment of legislative and executive authority by India’s judiciary is taking place, probably financial power is the last power that you have left”. And also: “Step by step, brick by brick, the edifice of India’s legislature is being destroyed”.
Such arguments were used by Indira Gandhi in the 1970s when she attacked the independence of the judiciary in the name of the people’s will — that she claimed she embodied after the 1971 election. The American social scientist Edward Shils, had shown, a long time ago, that populism is based on this opposition between the legitimacy of the elected politician and the legality enshrined in a Constitution whose custodians are the judges. Democracy without the rule of law quickly degenerates in mobocracy and eventually, even elections cannot be organised fairly. Which does not mean that the judiciary is always right, that the government of the judges is not posing a threat to democracy and that reforms should not take place in this domain too. But that will be the subject of another oped.
Postscript: The Supreme Court has informed the government that its collegium reiterated the 43 names that the government had just rejected. The arm-twisting game is turning into a tug of war which may damage a delicate institutional architecture.
मन और सेहत
वह कई महीनों से खराब गले व साइनस की समस्या से जूझ रहे थे। तमाम इलाज के बाद भी कोई खास फर्क नहीं लग रहा था। मगर जब मेडिटेशन का सहारा लिया, तो चमत्कारिक सुधार देखने को मिला। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया के विशेषज्ञ एलजे सोल की राय है कि भावनात्मक असंतुलन व संकल्प-विकल्पों के अनियंत्रित हो जाने से हमारे गले के कोमल तंतुओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। टेंपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज के एडवर्ड वीस अपने मेडिकल रिसर्च पेपर में बताते हैं कि भावनात्मक असंतुलन ग्रंथियों के स्राव को प्रभावित करता है और साथ-साथ हमारी म्यूकस मैम्ब्रेन को सर्दी के वायरस व एलर्जी के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देता है।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फिजिशियन व सर्जन एडमंड पी फाउलर कहते हैं, ‘परीक्षा के दौरान कई विद्यार्थी सर्दी-जुकाम के शिकार इसलिए होते हैं, क्योंकि परीक्षा का डर उनके भावनात्मक संतुलन को अव्यवस्थित कर देता है।’ क्रोध, चिड़चिड़ापन, नफरत और द्वेष भावनात्मक असंतुलन की निशानी है। इन विकारों से निजात पाने के लिए स्वयं को सद्भाव, क्षमा, प्रेम व शांति के सकारात्मक सुझाव दें। इन सुझावों को स्थायी बनाने में मेडिटेशन का नियमित अभ्यास बहुत उपयोगी है।
सकारात्मक चिंतन के पितामह कहे जाने वाले नार्मन विंसेन्ट पील की राय है, ‘भावनाएं उतनी ही असली हैं, जितने कि कीटाणु।’ अत: भावनाओं के कारण जो दर्द का एहसास होता है, वह बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न दर्द जितना ही काल्पनिक है। मनोविश्लेषकों का मानना है कि भावनात्मक असंतुलन के शिकार लोग किसी बीमारी से पीड़ित नहीं होते, बल्कि वे भावनात्मक असंतुलन से जूझ रहे होते हैं।
विनोद कुमार यादव
Date: 23-11-16
सोशल मीडिया से ताजा खबरों की दस्तक
ऐसे समय में, जब फेसबुक समेत सोशल मीडिया के लगभग सभी माध्यम झूठी और फर्जी खबरों की समस्या से जूझ रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो रहा है, जो बहुत उम्मीद बंधाता है। इस साल अगस्त में जब फेसबुक ने लाइव फीचर शुरू किया था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि कैसे फेसबुक में लाइव वीडियो फीचर का यह छोटा-सा ‘आइकन’ भारत को सिटिजन जर्नलिज्म की अगली पीढ़ी में ले जाने वाला है और टीवी पत्रकारिता के तौर-तरीके पर गहरा असर डालने वाला है। इस वक्त जब पूरा देश नोट बदलने के लिए एटीएम या बैंक के बाहर लाइन में लगा है, स्थिति की गंभीरता को दिखाने के लिए महज तस्वीरों से ही नहीं, बल्कि इस लाइव वीडियो का भी सबसे सटीक इस्तेमाल हो रहा है। अखबारों, टीवी चैनलों ने भी इस अवसर का फायदा उठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। नए नोट पाने या पुराने नोट निपटाने के लिए लाइन में लगे लोगों को दिखाने और उनकी प्रतिक्रिया को समझने के लिए फेसबुक लाइव फीचर एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी दौरान, नमक की कमी को लेकर फैली अफवाह को खत्म करने में भी लोगों ने इस फीचर का बखूबी इस्तेमाल किया, जिससे स्थिति खराब नहीं होने पाई।
फेसबुक का यह फीचर प्रयोगकर्ताओं को रियल टाइम में सीधे प्रसारण की सुविधा देता है। यह ठीक है कि पहले लोगों ने मजे के लिए लाइव होना शुरू किया, मगर धीरे-धीरे इसमें गंभीरता आनी शुरू हो गई है। इस फीचर के मानक गढ़ने और सीखने में फेसबुक के भारतीय उपयोगकर्ताओं ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया। जो यह भी बताता है कि देश नए मीडिया के प्रयोग के तौर-तरीके बहुत जल्दी आत्मसात कर रहा है। जिसे हम डिजिटल इंडिया कहते हैं, वह भले ही एक सरकारी प्रयास और नारा है, लेकिन सच यह है कि देश की युवा पीढ़ी डिजिटल बदलावों और औजारों को लेकर काफी सहज हो चुकी है। अब नए बदलाव की राह इसी सहजता से निकलेगी।
भारत में इस समय 15 करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक का उपयोग कर रहे हैं। अब आगे इस संख्या को लगातर बढ़ाते रहना फेसबुक की सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसी ही चुनौती देश में सक्रिय सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म की भी है। शोध बताते हैं कि लोगों का समाचार पाने का तरीका सोशल मीडिया के आने के बाद बदला है और वे समाचारों के लिए टीवी की बजाय सोशल नेटवर्किंग साइट्स की ओर रुख कर रहे हैं। फेसबुक के पास टेक्स्ट, तस्वीरें और वीडियो शेयर करने की व्यवस्था पहले से ही थी, पर लाइव वीडियो फीचर ने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है। सिटिजन जर्नलिज्म की अवधारणा में जिस गति की कमी सोशल मीडिया साइट्स में महसूस की जा रही थी, उसको लाइव वीडियो ने भर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि इसका असर हमारे समाचार टीवी चैनलों पर भी जल्द दिखेगा।
यह भी मुमकिन है कि खबरों को पाने का उनका सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया ही बन जाए। ओबी वैन से सीधा प्रसारण बहुत जल्द ही इतिहास हो जाने वाला है। असल में, यही एक ऐसा तत्व है, जो एक आम इंटरनेट प्रयोगकर्ता के पास नहीं था, इसलिए उसकी निर्भरता समाचार और सूचना पाने के लिए टीवी पर थी। अभी तक की तकनीकी व्यवस्था में सीधे प्रसारण के कारण टीवी ज्यादा विश्वसनीय था, पर अब वह दूरी भी खत्म हो गई है। इस बीच भारत में लगातार स्मार्टफोन की संख्या बढ़ती जा रही है, जो इस बात का द्योतक है कि फेसबुक का यह फीचर अभी और ज्यादा लोकप्रिय होगा और लोगों को अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए टीवी चैनल जैसे महंगे माध्यम की जरूरत नहीं होगी। उनके पास खुद का अपना माध्यम होगा।
बेशक इसके रास्ते में कई बाधाएं हैं। सबसे बड़ी बाधा इंटरनेट की गति है। 4जी तकनीक का विकास और विस्तार इसकी गति को कितना तेज कर सकता है? इससे भी बड़ी चुनौती नागरिक पत्रकारिता के नाम पर सामग्री की भरमार की है। सोशल मीडिया इस अराजकता से निकलकर सुगठित रूप में कैसे निखरेगा, यह कोई नहीं जानता। फिर इसे विश्वसनीयता कायम करने के लिए भी संघर्ष करना होगा।
मुकुल श्रीवास्तव, एसोशिएट प्रोफेसर ,लखनऊ विश्वविद्यालय (ये लेखक के अपने विचार हैं)
Date: 23-11-16
काम न मिलने के खतरे
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में अस्थायी नौकरियों और शून्य मजदूरी वाली नौकरियों की वजह से लोगों में गहरी चिंता घर करती जा रही है। शून्य मजदूरी वाली नौकरी उसे कहा जाता है, जिसमें नौकरी का कांट्रैक्ट तो होता है, मगर कामकाज मिलने की गारंटी नहीं होती। यह रोजगार देने वाली कंपनी पर निर्भर करता है कि वह उन कामगारों को बुलाए या नहीं। यह बिल्कुल दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों जैसी स्थिति होती है। इसके गंभीर नतीजों को देखते हुए अब अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने कहा है कि ऐसे वातावरण से न सिर्फ लोगों को कम मजदूरी पर या मजदूरी के बिना गुजारा करना पड़ता है, बल्कि उनमें कामकाज की असुरक्षा भी बढ़ती है। इसके अलावा, लोगों की क्षमता और प्रतिभा का भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। यह चलन गरीब और अमीर, दोनों तरह के देशों में बढ़ा है। अस्थायी नौकरियों और जीरो कांट्रैक्ट का असर महिलाओं, बच्चों और उन प्रवासियों की जिंदगी पर ज्यादा पड़ता है, जिन्हें किन्हीं मजबूरियों की वजह से अपना घर, स्थान या देश छोड़ना पड़ता है। ब्रिटेन में ही करीब तीन फीसदी कामगार ऐसी व्यवस्था के तहत काम करते हैं। आईएलओ की मांग है कि काम करने वाले लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिए, तभी वे सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं।
(संयुक्त राष्ट्र रेडिया में महबूब खान)