
25-10-2018 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date:25-10-18
Date:25-10-18
Here Come Robots
India must prepare its workforce for the automation revolution
TOI Editorials
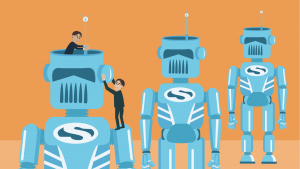
A recent survey based on data from secondary sources reveals that more than half of generic work profiles in India will face the risk of disruption over the next two years due to automation. The Teamlease Services study estimates that 52-69% of repetitive and predictive roles in sectors such as IT, financial services, manufacturing, transportation and packaging will be exposed to the risk of automation. However, this may not automatically imply job losses as new high-order jobs will be created simultaneously. In other words, greater adoption of artificial intelligence (AI) will likely see role changes in the workforce that would need higher specialisation and critical thinking.
So a financial analyst will be replaced by an adviser, a telemarketer by a marketing algorithm builder, and a retail salesperson by a retail adviser. But the question that needs to be asked is, is India preparing its workforce for such a transition? For, unless adequate investments are made on upgrading skill levels, the oncoming AI revolution will certainly lead to largescale job losses. In this direction, efforts should begin with school education itself with curricula preparing students for jobs of the future. In fact, we could take a leaf out of approaches being followed by countries such as China and Germany.
In China, there is a great push for AI education with plans to set up 50 AI colleges and research institutes by 2020 already in motion. Add to this China’s rise as a robotics powerhouse on the back of a ‘Maker Movement’ that encourages youngsters to take up making tech-intensive machines and robots. Similarly, some German states have introduced coding for high school students while some schools in Estonia are teaching programming to six-year-olds. All of this is in preparation for the future labour market. India, given its huge population, shouldn’t lag behind in riding the AI wave. Otherwise, its demographic dividend will soon become a demographic time bomb.
Date:25-10-18
Carrot and Stick
SC yields a little to those insistent on bursting crackers but cracks down on pollutants
TOI Editorials
With Supreme Court’s “balanced approach” to tackling pollution caused by firecrackers awaiting the challenge of implementation, governments must adopt a phased plan to give teeth to the verdict. Rather than go for an outright ban on sale of firecrackers which was attempted with mixed results last year, SC has ruled that only crackers with reduced emissions and “green crackers” can be sold. The court has also fixed narrow time slots of 8-10pm for bursting crackers on Diwali and other festivals.
Given that Diwali is just two weeks away it may be too late for course correction and for the Sivakasi-based industry to produce firecrackers subscribing to the new norms this season. Retailers are already liquidating their inventory before state action gathers pace. Preventing the sale of polluting firecrackers and ensuring that they are burst only during the specified time periods will test the capacity of police forces to the hilt. Supreme Court judgments have a tough time prevailing over traditions. The verdict allowing women to worship at Sabarimala couldn’t be implemented because of massive protests.
Similarly, last year’s ban on sale of firecrackers may have succeeded in ensuring a cleaner Diwali than previous years but cracker bursting was still widely prevalent. However, awareness can play a key role in triggering reform. Air quality indices from metro cities across India reveal a spurt in pollution during Diwali. The implications of smoke and sound produced by firecrackers for those suffering from respiratory and cardiovascular ailments and hypertension have generated public opinion. In north India, the combination of cracker emissions and stubble burning had produced a “gas chamber” effect in 2016, which was a wake-up call for many.
The recent emphasis on scientifically improving firecracker composition holds great promise. The development of “green crackers” with lower emissions and producing water particles that suppress dust and “electronic crackers” at CSIR labs must be adopted by the industry. Meanwhile, government must monitor compliance of Petroleum and Explosives Safety Organisation’s ban on antimony, mercury, arsenic and lead last year and SC’s order banning the use of aluminium and barium nitrate. Government also needs to crackdown on Chinese crackers, which are cheaper and no less toxic, and have made rapid inroads into Sivakasi’s market. With a phased multipronged plan and public participation, firecracker production, sale and use can be regulated. It is a test of state capacity and individual civic spirit.
Date:25-10-18
Comical Bureau Of Intrigue
CBI looks like a joke. Will GoI finally make it a statutory body?
Saubhik Chakrabarti is Associate Executive Editor, ET.
What is the world’s most unenviable top cop job now? Interim chief, the Central Bureau of Investigation (CBI). Nageshwar Rao, picked by the Prime Minister-led Appointments Committee of the Cabinet, has the toughest remit in any public service – to stop people from laughing at the institution he leads. The agency can now fairly be called the Comical Bureau of Intrigue, with its two erstwhile senior most officers, director Alok Verma and special director Rakesh Asthana, sent on leave, while different courts deal with disturbingly dramatic plaints made by both.
These are golden days for reporters on the CBI beat, as all sides will inevitably provide more strategic leaks. Those details will have a bearing on the specific controversies framing the CBI mess. But as people outside the government-media complex consume news reports on a Doon and St Stephens educated meat exporter alleged to be close to those in the opposition and a sent-on-leave CBI bigshot who is alleged to be close to those in power, to name only two characters in a multi-starrer burlesque, the general and justified response will be to laugh at the utter absurdity of it all.
The government is also squarely responsible because all of this has happened under its watch. Its decision to send away both warring CBI officers and ask a special investigation team (SIT) to probe allegations and counter-allegations, while entirely sensible, doesn’t even begin to address the question why the Verma vs Asthana dramedy was allowed to play out for as long as it did.
BJP has made a consistent claim since 2014, when it stormed into power, that one of the defining differences between its government and the one run by Congress is that the latter was prone to dysfunction while the former is always in charge. At least on the CBI question, that claim is in tatters. The really troubling perceptional question for BJP here is not so much whether it was using CBI as a political tool. That charge has been made against Congress for far longer. What is hurting and will likely hurt BJP is popular perception that its government appeared helpless as the CBI story moved from chaos to farce.
Therefore, countering the Congress charge that Verma was “targeted” because he was apparently “thinking” of a Rafale probe may be politically necessary right now for BJP. It may also be relatively easy to do so – how does Congress know what Verma was thinking, is the obvious retort. But the bigger political job for BJP is to convince people that on the CBI issue, it is back in control. Because for the first time since 2014, and weeks away from the beginning of a long election cycle, the opposition has the chance, if it is minimally clever, to build a narrative that this government, too, is prone to dysfunction.
So, BJP will hope that the SIT will keep Verma and Asthana busy, that courts won’t upend its interim arrangement for CBI, that Rao will step up to the plate and appear as an officer in charge, and that CBI investigations into non-CBI corruption cases will make news. Note, however, that there are many things here that the government does not control or may not be able to control. For example, one known unknown right now is how the Supreme Court will respond to the ex-CBI chief being sent on leave. The other problem can be whether the accused in various CBI high profile cases supervised by Asthana will benefit from corruption charges against him.
So, the perception of chaos may not necessarily go away. Therefore, BJP needs a politically solid and institutionally impeccable talking and action point, a real solution that will help restore CBI’s institutional credibility and prove that the government is back in charge.
That solution, as many ex-top cops and commentators with domain knowledge of law enforcement affairs have said multiple times, is to make CBI a statutory body through a fresh law. CBI functions under clauses that draw institutional validity from the Delhi Special Police Establishment Act. Many Supreme Court efforts to institute operational independence for CBI have essentially failed because the agency, as its status is now, is neither de jure nor de facto immune from political interference.
The Election Commission, the Securities and Exchange Board of India, the Telecom Regulatory Authority of India, the Comptroller and Auditor General are all constitutional or statutory bodies. That basically means political interference is difficult in these institutions. So should be the case for CBI. CBI also draws its senior officers from the Indian Police Service (IPS) and many IPS officers who man CBI – let’s put it politely – have close encounters with politics. Therefore, CBI as a statutory body should also be mandated to draw its cadre from a wide pool of talent and given its own budget. That’s the best way to secure its future, make it a law-backed autonomous investigative agency that attracts quality candidates because the job offers enormous prestige, good pay and real professional independence.
Were the government to announce it is starting the process of writing such a law to create a new, improved CBI, and that its decision is directly related to the current mess at the agency, no matter how Verma vs Asthana plays out, BJP will always have a winning talking point. Every critic will applaud the decision. Congress will find it pretty much impossible to oppose the decision on principle. But will it happen? Will this government, or any government run by other parties, want to make CBI a statutory body? Let’s put it this way. It would be great for India if it happens. It would also be greatly surprising if it does.
![]() Date:25-10-18
Date:25-10-18
अंदरखाने ही करनी होगी शुरुआत न्यायपालिका में सुधार की
एम जे एंटनी
नौ महीनों तक चले थपेड़ों के बाद उच्चतम न्यायालय में आई सापेक्षिक शांति के बीच नए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने न्यायिक व्यवस्था को परेशानी में डालने वाली बुराइयों को दूर करने के लिए मौलिक सुधारों का वादा किया है। आने वाले कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा कि न्यायमूर्ति गोगोई अपने 13 महीनों के कार्यकाल में इस बड़े काम को कैसे पूरा करेंगे?
फिलहाल देश में इस समय तीन करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, 24 उच्च न्यायालयों में 43 लाख मामले और खुद उच्चतम न्यायालय में भी 54,000 से अधिक मामले विचाराधीन हैं। निचली अदालतों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 22,444 है जिनमें से 5,223 स्थान रिक्त हैं। उच्च न्यायालयों में भी 427 पद खाली पड़ हुए हैं जो कुल स्वीकृत पदों 1,079 का 40 फीसदी हैं। भारत में इस समय हरेक 10 लाख आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या महज 19 है जबकि विधि आयोग ने वर्ष 1987 में ही इस अनुपात के 50 रहने को स्वस्थप्रद स्थिति बताया था। हालांकि लंबित मुकदमों के प्रबंधन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के इस्तेमाल की सलाह जैसे पेचीदा मामलों को विशेषज्ञों पर ही छोड़ देना चाहिए लेकिन लंबे समय तक अदालतों के चक्कर लगाते रहे शख्स भी कुछ सुझाव दे सकते हैं। खुद न्यायाधीश भी कामकाज संबंधित निर्देश देकर इन सुधारों का आगाज कर सकते हैं।
पहला, उच्चतम न्यायालय की संकल्पना एक संवैधानिक न्यायालय के तौर पर की गई थी जो कानूनों की व्याख्या से संबंधित मामले देखेगा। लेकिन पिछले दशकों में यह एक अपीलीय अदालत बनकर रह गया है जो सेवा में प्रोन्नति, किरायेदारी और जमीन विवाद जैसे साधारण मामले देखता है। ये मामले संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आते हैं जिसमें विशेष अनुमति याचिका की शक्ल में अपील की इजाजत दी गई है। विशेष अनुमति याचिकाओं की संख्या ने रिट याचिकाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। लिहाजा इस न्यायाधिकार के इस्तेमाल पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए।
दूसरा, न्यायालय को महीनों तक खिंच जाने वाली सुनवाई को सीमित करना चाहिए। आधार मामले में ही वकीलों को अपना पक्ष रखने के लिए तीन महीनों के दौरान 38 दिवस दिए गए थे। संभवत: उसी समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को यह अहसास हुआ कि सेवानिवृत्ति के पहले उनके पास कुछ हफ्ते ही रह गए हैं और आरक्षण, व्यभिचार, समलैंगिक अधिकार एवं मंदिर प्रवेश जैसे ऐतिहासिक महत्त्व के तमाम मामले उनकी अदालत में लंबित पड़े हैं। ऐसे में उन्होंने सभी मामलों में तेजी दिखाई और हरेक पर बहस के लिए तीन-चार दिन ही दिए। यह घटना दिखाती है कि मुख्य न्यायाधीश केवल न्यायाधीशों को मामले आवंटित करने वाला रोस्टर ही नहीं बल्कि तारीख एवं घड़ी का मास्टर भी होता है।
इसके पहले बहस करने वाले वकीलों को लंबा वक्त देने के पीछे यह तर्क दिया जाता था कि भारतीय अदालतें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बजाय ब्रिटिश प्रणाली का अनुसरण करती हैं। अमेरिकी अदालत हरेक पक्ष को अपनी दलील रखने के लिए महज आधे घंटे का वक्त देती है। अमेरिका में न्यायाधीशों की मदद के लिए कानूनी क्लर्क होते हैं जो काफी खोजबीन करते हैं। लेकिन इस दलील का अब कोई आधार नहीं रह गया है। भारत में भी अदालत के भीतर एक शोध प्रकोष्ठ बना हुआ है। इसके अलावा न्यायाधीशों को इंटर्न से भी मदद मिलती है। इसलिए बहस के समय में कटौती की जा सकती है। अगर वकील अपने मुवक्किलों को प्रभावित करने या अधिक फीस वसूलने के लिए बहस को लंबा खींचते हैं तो उन पर अतिरिक्त समय के अनुपात में दंडात्मक शुल्क लगाया जा सकता है।
सुनवाई में खलल डालने की बुराई सुविदित है और अब यह फिल्मों का पसंदीदा दृश्य भी बन गया है। इसे नियंत्रित करना न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र में है लेकिन वकीलों की चतुराई और न्यायाधीशों की सुस्ती ने अदालती कार्यवाही को काफी प्रभावित किया है। आम धारणा है कि जनहित याचिकाएं अब बेलगाम घोड़े के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। कुछ समय पहले एक कृषि विशेषज्ञ ने प्राइमरी क्लास में पढऩे वाले बच्चों को संविधान का समूचा पाठ सिखाने की मांग की थी। इसी तरह एक वकील नकदी मुद्रा को खत्म करने की मांग कर रहे थे। एक नागरिक ने तो उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर स्वतंत्रता से पहले के सभी कानूनों को खत्म करने की मांग रखी थी। इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था लेकिन इसी तरह की याचिकाएं अब भी सूची में दर्ज हैं।
भले ही अदालत हरेक नागरिक के लिए खुली है लेकिन न्यायाधीशों के कमरों में खड़ी बेतरतीब भीड़ इसकी प्रतिष्ठा में कोई इजाफा नहीं करती है। अक्सर बुजुर्गों को कार्यवाही देखने के लिए आने वाले लोगों के बीच से होकर अदालत के कक्ष तक पहुंचने में जद्दोजहद करनी पड़ती है। कुछ जिला अदालतों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होती है जिनके मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होते हैं। नए मुख्य न्यायाधीश के सामने एक बड़ी चुनौती न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया का खाका तय करने की है। यह प्रस्ताव दो साल से लटके होने से शीर्ष अदालत और सरकार के बीच खींचतान की नौबत भी आ गई। लेकिन मौजूदा सरकार का कार्यकाल करीब आने से कॉलेजियम के सुझावों को खारिज किए जाने की संभावना नहीं रह गई है। इस मोर्चे पर मुख्य न्यायाधीश को थोड़ी राहत मिली है। जब देश नई सरकार के लिए इंतजार कर रहा हो तो न्यायपालिका में सुधारों की शुरुआत उसके भीतर से ही शुरू हो सकती है।
Date:25-10-18
कब तक रुलाएगा प्याज !
संपादकीय
प्याज की कीमतों में अस्थिरता की समस्या एक बार फिर हमारे सामने आ खड़ी हुई है। इस बार उपलब्ध प्याज आपूर्ति के कुप्रबंधन के अलावा कोई बड़ा कारण नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के लासलगांव स्थित प्याज की सबसे बड़ी मंडी में बीते एक सप्ताह में प्याज की थोक कीमतें दोगुनी हो गई हैं।
देश के कई इलाकों में इसकी खुदरा कीमतों में इससे भी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। यह स्थिति कुछ वर्ष पहले से एकदम उलट है जब प्याज किसानों को अपनी उपज सड़कों पर फेंकनी पड़ी थी क्योंकि इसकी कीमतों में भारी गिरावट आ गई थी। बाजार सूत्रों का कहना है कि फिलहाल कीमतों में इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र में कमजोर बारिश से प्याज की फसल खराब हुई है। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में प्याज की खेती अच्छी है। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 में प्याज की फसल औसत से बेहतर रहने का अनुमान जताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि बुआई के रकबे में इजाफा हुआ था। एक सप्ताह में प्याज की नई फसल आ जाएगी। चूंकि कई महत्त्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं इसलिए केंद्र सरकार ने नेफेड और मदर डेयरी जैसे संस्थानों को रियायती दर पर प्याज बेचने का आदेश देने में जरा सा भी वक्त नहीं गंवाया। हालांकि उसके इस कदम से किसानों के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। हो सकता है वे भविष्य में उत्पादन बढ़ाने से दूरी बनाएं।
प्याज उन फसलों में शामिल है जिन्होंने हाल के वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वर्ष 2000 में जहां प्याज का सालाना उत्पादन करीब 50 लाख टन था, वह अब 2.2 करोड़ टन तक पहुंच चुका है। इसके बावजूद प्याज की कीमतों में अस्थिरता की समस्या बनी हुई है क्योंकि सरकारी नीतियां इसका समर्थन नहीं करतीं और मौजूद आपूर्तियों का न तो ठीक से प्रबंधन होता है और न ही वितरण। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है सरकार की बिना सोची समझी प्रतिक्रिया। वह कभी भंडारण की सीमा तय कर देती है तो कभी कारोबारियों पर छापे मारे जाते हैं, कभी अचानक आयात-निर्यात के नियम बदल दिए जाते हैं। ऐसे ही कई मनमाने कदम उठाए जाते हैं। इससे बाजार में बेवजह अफरातफरी पैदा होती है।
एक बात की अक्सर अनदेखी कर दी जाती है कि आपूर्ति क्षेत्र के झटके अक्सर अल्पावधि के होते हैं क्योंकि प्याज की खेती रबी और खरीफ दोनों मौसमों में होती है। चूंकि इसकी मांग पूरे वर्ष बनी रहती है इसलिए हर मौसम के उत्पादन के एक हिस्से का संरक्षण जरूरी है ताकि जरूरत पडऩे पर मांग पूरी की जा सके। खेद की बात है कि इस जरूरी भंडारण को जमाखोरी का नाम देकर हतोत्साहित किया जाता है। जरूरत यह है कि उपज को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने और मुनाफे के लिए जमाखोरी में भेद किया जाए। अल्पावधि के लिए प्याज का भंडारण करना न तो कठिन है, न ही महंगा। प्याज को सुखाना और उसका पेस्ट बनाना ऑफ सीजन में उपलब्धता सुनिश्चित करने के अन्य सस्ते जरिये हैं।
प्याज की खेती को भी चंद राज्यों से बाहर ले जाने की जरूरत है। अभी अधिकांश आपूर्ति महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान से आती है जबकि प्याज की खेती देश के अधिकांश राज्यों में हो सकती है। इससे चुनिंदा राज्यों पर निर्भरता कम होगी और देश भर में इसकी सहज उपलब्धता हो सकेगी। इसके अलावा उत्पादन संभावनाओं और कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए भी समझदारी भरी व्यवस्था करनी होगी। इन समस्याओं को हल करने के लिए बहुकोणीय नीति तैयार करनी होगी। तभी प्याज उत्पादन में स्थिरता आएगी और उसकी कीमत ऐसी होगी जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए हितकारी हो।
सरकार के ‘हस्तक्षेप’ से और उलझा सीबीआई का मामला
संपादकीय
केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख केवी चौधरी के सुझाव पर केंद्र सरकार ने सीबीआई की साख बहाली के लिए जो कदम उठाए हैं वे नाकाफी हैं। उससे मामला और बिगड़ता जा रहा है। निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजकर संयुक्त निदेशक नागेश्वर राव को कमान देने पर कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। सवाल संवैधानिक भी हैं और राजनीतिक भी। संवैधानिक सवाल यह है कि निदेशक का कार्यकाल दो साल के लिए होता है। उसे बर्खास्त वह समिति ही कर सकती है, जो उसे नियुक्त करती है। उस समिति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। हालांकि वर्मा को बर्खास्त नहीं किया गया है लेकिन, छुट्टी पर भेजे जाने के सवाल पर वे सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। विपक्ष ने आलोक वर्मा की ओर से मोर्चा संभाल लिया है और सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वह विशेष निदेशक अस्थाना का पक्ष ले रही है।
सीबीआई की इमारत की न सिर्फ 10वीं-11वीं मंजिल को सील कर दिया गया है बल्कि 13 अफसरों को इधर से उधर किया गया है। इसमें दोनों गुटों के अधिकारी हैं लेकिन, वर्मा के करीबी अजय बस्सा को पोर्ट ब्लेयर भेजे जाने ने स्पष्ट कर दिया है कि उन अधिकारियों को ज्यादा प्रताड़ित किया गया है जो अस्थाना के विरुद्ध जांच कर रहे थे और जिन्होंने उनसे जुड़े डीएसपी देविंदर कुमार को पकड़ा था। उधर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है और जो भी कार्रवाई की गई है वह केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर की गई है। आयोग की निगरानी में ही सीबीआई काम करती है और उसी के सुझाव पर एक एसआईटी भी बनाई जा रही है, जो वर्मा और अस्थाना पर लगे आरोपों की जांच करेगी। फिर भी सार्वजनिक धारणा यही बन रही है कि अस्थाना ने सीबीआई में महत्वपूर्ण जांच हथियाकर गड़बड़ियां की हैं और सरकार उन्हें बचा रही है। लगता है कि सीबीआई की साख को बहाल करने का यह अस्थायी उपाय ज्यादा कारगर नहीं होगा और अगर सरकार समय रहते लोकपाल नामक संस्था को कायम करके सीबीआई को उसके मातहत लाए तो देश और संस्था दोनों का भला होगा।
जांच एजेंसी पर दाग अच्छे नहीं
सरकार ने सीबीआई के दोनों शीर्ष अफसरों को छुट्टी पर भेजकर बिलकुल ठीक किया। हालांकि नुकसान तो पहले ही हो चुका है।
भवदीप कांग , (लेखिका वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार हैं)

पिछले तकरीबन पांच साल से सीबीआई अंदरूनी स्कैंडलों, विवादों में उलझी है और इससे देश की इस शीर्ष जांच एजेंसी की निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता पर भी सवाल उठने लगे हैं। यह तो तय लगता है कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजने और एम. नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाए जाने के बाद भी यह विवाद थमने वाला नहीं है। वर्ष 2014 में एनडीए भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम छेड़ते हुए केंद्र की सत्ता में आया था। पहले भाजपा (और बाद में आम आदमी पार्टी) को उस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का लाभ मिला, जिसने मनमोहन सरकार के पतन की इबारत लिखने में अहम भूमिका निभाई थी। केंद्र की भाजपा-नीत सरकार को अपनी ‘स्वच्छ छवि के मद्देनजर कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए थे, जिससे सीबीआई की कार्यप्रणाली निर्विघ्न और ‘साफ-सुथरी बनाना सुनिश्चित होता।
वर्ष 2014 के महासमर से पूर्व यूपीए के इर्द-गिर्द निर्मित भ्रष्टाचार के घने कुहासे में सीबीआई का भी योगदान था। यूपीए सरकार द्वारा नियुक्त किए गए लगातार दो सीबीआई निदेशक शक के दायरे में आए। वर्ष 2010-12 के दौरान सीबीआई प्रमुख रहे एपी सिंह मांस कारोबारी और कथित हवाला रैकेटियर मोइन कुरैशी के साथ करीबियों के चलते शक के घेरे में रहे। अलबत्ता, आगे चलकर वे संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सदस्य भी बने। वहीं सिंह के बाद सीबीआई निदेशक बने रंजीत सिन्हा पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। एनडीए के सत्ता में आने के छह-सात महीने बाद सीबीआई निदेशक के रूप में सिन्हा का कार्यकाल (दिसंबर 2014 में ) समाप्त हो गया। वहीं सिंह को भी आयकर विभाग द्वारा उन्हेंव उनकी पत्नी के नाम नोटिस जारी किए जाने के बाद (जनवरी 2015 में) यूपीएससी से हटना पड़ा। वर्ष 2017 में उसी जांच एजेंसी ने इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसके कभी ये मुखिया रहे थे।
वर्ष 2017 में आलोक वर्मा की सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति चौंकाने वाली थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस में रहते हुए उनकी छवि एक ‘सौम्य पुलिस अफसर की थी। किंतु सीबीआई निदेशक बनने के बाद उन्होंने राकेश अस्थाना के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, जिन्हें सियासी रूप से शक्तिशाली समझा जाता था। जब सरकार ने राकेश अस्थाना को सीबीआई के विशेष निदेशक के तौर पर पदोन्न्त करने का फैसला किया, तब वर्मा ने इस पर सख्त ऐतराज जताया था। वर्मा का तर्क था कि जब अस्थाना खुद स्टर्लिंग बायोटेक केस में जांच के दायरे में हैं, तब उन्हें कैसे इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि स्टर्लिंग बायोटेक एक फार्मा कंपनी है, जिसके मालिक संदेसरा बंधु बैंक से धोखाधड़ी के एक बड़े मामले के बाद देश से फरार हो गए। यह साफ है कि अस्थाना को वर्मा के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा था। उन्हें वर्ष 2016 में उस वक्त सीबीआई का अंतरिम निदेशक भी बनाया गया था, जब तत्कालीन निदेशक अनिल सिन्हा के रिटायर होने से ऐन पहले इस संस्था में नंबर दो की पोजिशन पर रहे रूपक कुमार दत्ता का अचानक तबादला कर दिया गया।
बहरहाल, अस्थाना के मामले में यह तो लगता है कि वह शुरुआत से ही सीबीआई विशेष निदेशक के रूप में अच्छा विकल्प नहीं थे। आखिर देश की शीर्ष जांच एजेंसी होने के नाते सीबीआई को संदेह से परे होना चाहिए। भ्रष्टाचार की हल्की-सी आहट से भी इस संस्था की साख को धक्का पहुंचता है। एनडीए सरकार के पास इस गंदगी को साफ करने का मौका था, लेकिन इसके बजाय उसने भी विवादित अफसरों को संदेह का लाभ देने के यूपीए मॉडल पर ही चलना पसंद किया। कई ऐसी बातें हैं, जिनसे लगता है कि अस्थाना भाजपा के लिए सिरदर्द बन गए हैं। पहली बात तो यह कि उन्हें भाजपा नेताओं का करीबी माना जाता है। दूसरी बात, उन्हें सीबीआई के तत्कालीन निदेशक द्वारा भ्रष्टाचार के आधार पर विरोध के बावजूद विशेष निदेशक नियुक्त किया गया। तीसरी बात, उनके खिलाफ घूस लेकर मोइन कुरैशी का केस बंद करने की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया। पीएमओ ने दोनों शीर्ष अफसरों (वर्मा और अस्थाना) को छुट्टी पर भेजकर बिलकुल ठीक किया, लेकिन नुकसान तो पहले ही हो चुका है।
गौरतलब है कि अस्थाना को वर्ष 2016 में सीबीआई में लाए जाने से पहले ही लुटियंस दिल्ली के गलियारों में उनकी स्टर्लिंग बायोटेक के संदेसरा बंधुओं से कथित नजदीकियों के चर्चे आम थे। इसी तरह सिंह के मांस कारोबारी मोइन कुरैशी से कनेक्शन के बारे में भी मीडिया द्वारा उनके ब्लैकबेरी संदेशों के आदान-प्रदान को उजागर करने से पहले ही सब जानते थे। रंजीत सिन्हा के भी सीबीआई की निगरानी में रही कंपनियों के एजेंटों से रिश्ते कोई छुपी हुई बात नहीं थे। यदि इन तमाम मामलों पर दिल्ली के कॉफी शॉप में भी लोग गपशप करते रहते थे, तो ऐसे अफसरों को आखिर नियुक्त ही क्यों किया गया? समस्या यह है कि सरकार किसी अफसर का चयन करते वक्त उसका सर्विस रिकॉर्ड ही देखती है, उसके बारे में चल रही चर्चाओं पर गौर नहीं करती, जो बाद में सही भी साबित हो सकती हैं।
सीबीआई में तुरंत आमूलचूल बदलाव की दरकार है। सरकार द्वारा ‘बेदाग अफसरों का चयन सुनिश्चित करने का एक तरीका यह हो सकता है कि नियुक्ति प्रक्रिया बदली जाए। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसे निकाय के प्रमुख अफसरों के चयन में पारदर्शिता की खातिर यह किया जा सकता है कि अमेरिकी शैली की ‘कन्फर्मेशन हियरिंग्स या सुनवाइयों के जरिए इनकी नियुक्तियां हों। एक संसदीय समिति ऐसी सुनवाइयां आयोजित कर सकती है, जिसमें उम्मीदवारों से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जो इस पद हेतु उनकी उपयुक्तता स्थापित कर सकें। ऐसी सुनवाइयों के दौरान हितों के टकराव कोई मामला या जानकारी सामने आ सकती है, जो सर्च कमेटी के लिए उपलब्ध नहीं होती। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सीबीआई में जनता का भरोसा बहाल करने के लिए ऐसे ही सख्त उपायों की जरूरत है।
ऐसी किसी एजेंसी का राजनीतिकरण करने से समस्या यह है कि इसके अफसर राजनीतिक लड़ाइयों में एक पार्टी बन जाते हैं और इससे इसकी कार्यप्रणाली पर असर पड़ता है। यह महज दो शीर्ष अफसरों के मध्य अहं के टकराव का मामला नहीं, बल्कि सरकार के भीतर कहीं बड़ी लड़ाई की प्रतिध्वनि है। प्रधानमंत्री को न सिर्फ इस कॉप बनाम कॉप ड्रामे का अंत करना होगा, बल्कि सीबीआई को इस तरह पुनर्संयोजित करने की राह भी तलाशनी होगी, जिससे यह निष्पक्ष और प्रभावी जांच कार्रवाइयां करने में सक्षम बन सके।
कौन किसकी जांच करे
अरुण त्रिपाठी
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1941 में बनी विशेष पुलिस फोर्स को आजाद भारत की रियासतों के भ्रष्टाचार की निगरानी के लिए तैयार करने का सपना देखा था। वह जानते थे कि रसूखदार लोग किस प्रकार अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके न सिर्फ बड़े-बड़े अपराध करते हैं, बल्कि बचकर निकल भी जाते हैं। इसलिए उन पर निगरानी के लिए एक केंद्रीय एजेंसी जरूरी है। आज देश के भीतर फिर वैसे रसूखदार और भ्रष्ट लोगों की बहुतायत है। हालांकि पटेल के निधन से वह काम अधूरा छूट गया और उसे पूरा होने में अगले 16 साल लग गए। आज उसी केंद्रीय एजेंसी की जबरदस्त छीछालेदर सामने आई है। मंगलवार के अखबारों के वे शीर्षक याद रखे जाएंगे कि ‘‘सीबीआई ने सीबीआई पर छापा डाला’। जिन अखबारों ने बचते हुए मामले को उठाया, उनके शीर्षक हैं कि नम्बर एक और नम्बर दो की जंग तेज हुई। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि सीबीआई निदेशक अपने ही विशेष निदेशक पर तीन करोड़ रु पये से ऊपर की रिश्वत लेने के आरोप में एफआईआर करे और विशेष निदेशक केंद्रीय सतर्कता आयोग और कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर आरोप लगाए कि निदेशक ने इसी मामले में दो करोड़ रु पये की रिश्वत ली है। इससे भी विडंबना की बात है कि एफआईआर के बावजूद विशेष निदेशक गिरफ्तार नहीं हुआ।
डीएसपी पकड़ लिया गया जबकि सीबीआई जब किसी लोकसेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दायर करती है, तो गैर-जमानती मामला बनता है, और उसे गिरफ्तार तो किया ही जाता है। कई पुलिस अधिकारी और सिपाही तो सौ रु पये की रिश्वत पर पकड़ लिए जाते हैं। इसलिए अगर कभी सीबीआई के अधिकारी बीआर लाल ने कांग्रेसी लीपापोती से ऊब कर सवाल पूछा था कि सीबीआई का मालिक कौन-एक नग्न सच्चाई (हू ओन्स सीबीआई नैकेड ट्रुथ) तो आज यह सवाल पूछा जा सकता है कि सीबीआई किसकी जांच करे-अपनी या दूसरों की’ क्योंकि सीबीआई का मालिक कौन?, इसमें तो कोई भ्रम नहीं है। सीबीआई का मालिक वही है, जो देश की सत्ता का मालिक है। चाहे वह नेता हो या परोक्ष रूप से पूंजीपति। बल्कि कहा जाए कि सबदा मालिक एक है, तो भी अतिश्योक्ति नहीं होगी। लेकिन सवाल है कि सीबीआई के भीतर से पटाखों की तरफ फूटने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों की पहले जांच होनी चाहिए या बाहरी व्यक्तियों और संस्थाओं की। विधिशास्त्र की बड़ी मशहूर सूक्ति है, ‘‘वन हू वान्ट्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी’ यानी जो किसी का अपराध पकड़ने का काम कर रहा है, उसे स्वयं अपराधी नहीं होना चाहिए। अपराध की जांच करने वाला ही संदिग्ध है, तो जांच पर किसको भरोसा होगा। इसलिए अगर यूपीए सरकार के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने टूजी और कोयला घोटालों की जांच के समय सीबीआई पर तंज कसते हुए कहा था कि यह तो पिजड़े में बंद तोता है यानी उसका मालिक जो रटाएगा वही बोलेगा। लेकिन आज पिजड़े में बैठे तोते आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं।
उन्हें मालिक का ख्याल ही नहीं रहा है या उसमें एक अपने को मालिक के ज्यादा करीब समझता है, तो दूसरे को अपनी ताकत के इस्तेमाल की पड़ी है। सीबीआई विशेष पुलिस बल के रूप में गठित हुई थी। बाद में इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत एक संस्था का रूप दिया गया। उसके जिम्मे आर्थिक अपराध, विशेष अपराध, भ्रष्टाचार के मामले और बड़े लोगों के मामले दिए गए। वे ऐसे मामले होते हैं, जिन पर राज्य की पुलिस दबाव में आ जाती है, या अपने रोजमर्रा के कामों से ऊपर उठकर वह उन पर उतना समय और विशेषज्ञता नहीं लगा पाती। लेकिन बीआर लाल ने अपनी किताब ‘‘हू ओन्स सीबीआई’ में बता दिया है कि वह राजनीतिक दबाव से किस कदर पायमाल है। इसकी सबसे ज्यादा लाचारी सामने आई जब उसने बोफोर्स तोप सौदे की जांच अपने हाथ में ली। उस समय के अखबार कितनी खबरों से भरे पड़े थे कि सीबीआई बोफोर्स के दस्तावेज लाने स्विटजरलैंड गई, स्वीडन गई, लंदन गई।
उसके बाद तमाम फोटो छपते थे जिनमें बक्शों में बोफोर्स के कागज लेकर सीबीआई आ रही है, और हाई कोर्ट में जमा कर रही है। सीबीआई की वह जांच एक मजाक बन गई क्योंकि उसमें से कुछ निकला नहीं। शायद इसीलिए कांग्रेस का पक्ष लेते हुए चंद्रशेखर कहा करते थे कि बोफोर्स की जांच तो कोई दरोगा भी कर सकता है, उसके लिए सीबीआई की क्या जरूरत है। आज इस प्रमुख संस्था में मचे घमासान से साबित हो गया है कि उसमें किसी विशेष साख और प्रतिबद्धता के अधिकारी नहीं, एक प्रकार के दरोगा ही बैठते हैं, जो अपनी तरक्की के लिए किसी को फंसा देते हैं, और किसी को बख्श देते हैं। सीबीआई ने न सिर्फ बोफोर्स की दलाली में शामिल इतालवी व्यापारी ओक्टावियो क्वात्रोच्चि को विदेश जाने की इजाजत दे दी, बल्कि हाल में बैंकों को करोड़ों का चूना लगाने वाले व्यापारी विजय माल्या के लुक-आउट नोटिस को भी उसी तरह नरम कर दिया। आतंकियों को चंदा पहुंचाने वाले हवाला रैकेट में फंसे लालकृष्ण आडवाणी, विद्याचरण शुक्ल, पी शिवशंकर, मोती लाल वोरा और यशवंत सिन्हा को भी सीबीआई की जांच में बेदाग करार दिया गया और अब तक सीबीआई की जांच में न मायावती फंस सकी हैं, न मुलायम।
टूजी मामला भी छूट ही गया है। सोहराबुद्दीन का विवाद भी इसकी विफलता का उदाहरण है। सीबीआई की सफलता चारा घोटाले के रूप में लालू यादव को लपेटने के रूप में जरूर देखी जा सकती है। उसके मामलों में सजा पाने की दर 67 प्रतिशत है, और यह उपलब्धि अच्छी ही कही जाएगी। हालांकि सीबीआई जैसी संस्था का आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जाना एक बड़ी विडंबना है। उसे कितना और कैसे लाया जाए इस बारे में भी सोचना होगा। सवाल है कि हमें सीबीआई जैसी संस्था को देश में कानून के राज को मजबूत करने के लिए रखना है, या राजनीतिक बदले की भावना से काम करने के लिए। इसकी साख बहाल करनी है तो इसे 2013 के कानून के तहत तत्काल लोकपाल जैसी संस्था बनाकर उसके मातहत करना चाहिए। इसे संवैधानिक दरजा देकर प्रतिष्ठा देनी होगी। नहीं तो गुवाहाटी हाईकोर्ट की तरह कोई अदालत उसे असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। कई सालों के अनुभवों और आंदोलनों के बाद उसे लोकपाल के साथ जोड़ना एक दूरदृष्टि का सुझाव है, और उसे तत्काल लागू करना चाहिए।
हथियारों की होड़
संपादकीय
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से परमाणु हथियार बनाने का एलान कर दुनिया को सकते में डाल दिया है। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका ने रूस के साथ तीन दशक पुरानी जो संधि कर रखी है, उसे अब खत्म कर दिया जाएगा। जाहिर है, अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐसा एकतरफा एलान दुनिया की नींद उड़ाने वाला है। अगर ऐसा होता है तो साफ है कि अमेरिका फिर से छोटी और मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलें बनाएगा। वर्ष 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन और तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने परमाणु हथियार नहीं बनाने को लेकर एक संधि की थी, ताकि दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ खत्म की जा सके। इसके तहत दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि साढ़े पांच हजार किलोमीटर तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों के निर्माण, तैनाती और इनके परीक्षण पर पाबंदी रहेगी। अगर अमेरिका और रूस के बीच यह संधि खत्म हो जाती है तो नतीजे दुनिया को जोखिम में डालने वाले होंगे।
परमाणु हथियारों की दुनिया में दबदबा बनाए रखने की अमेरिका की मंशा जगजाहिर है। हथियारों के बल पर ही अमेरिका दुनिया में दादागीरी कर रहा है। लेकिन रूस और चीन जैसे देश उसके लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। रूस और चीन को निशाना बनाते हुए अमेरिका ने इस साल एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है और रूस भी इसमें कटौती करने को राजी नहीं है। तब रूस और चीन दोनों ने इस रिपोर्ट पर एतराज जताते हुए अमेरिका को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि वह पहले अपने परमाणु हथियार कम करे। रूस ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या कम करने से साफ मना कर दिया था और इसे अमेरिका का रूस विरोधी रुख करार दिया था। अनुमान है कि रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रूस और अमेरिका के पास अभी चौदह हजार से ज्यादा परमाणु हथियार हैं जो दुनिया को कई बार तबाह करने की क्षमता रखते हैं। यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है।
परमाणु हथियारों की होड़ रोकने के लिए कोशिशें काफी पहले से होती रही हैं। महाशक्ति कहे जाने वाले देश इसके केंद्र में रहे, जो अपने हितों पर चोट नहीं पहुंचने देना चाहते थे। इसके लिए पिछले कई दशकों में संधियां हुर्इं, प्रतिबद्धता भी जाहिर की गई और कुछ देशों के खिलाफ प्रतिबंध जैसे कदम भी उठाए गए। लेकिन यह सब छलावा ही साबित हुआ और ताकतवर देश हथियार बनाने, बेचने और जमा करने से बाज नहीं आए। इसी का नतीजा है कि परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज सवाल यह उठ रहा है कि कौन देश हथियार बनाए और कौन नहीं। हर देश को अपनी संप्रभुता की रक्षा और सीमाओं व नागरिकों सुरक्षा के लिए वे सारे कदम उठाने का अधिकार होना चाहिए, जो दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देशों को हैं। ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को परमाणु शक्ति संपन्न होने का उतना ही अधिकार है जितना अमेरिका और दूसरे देशों को है। लेकिन समस्या की जड़ यही है कि अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देश परमाणु शक्ति से संपन्न बने रहना चाहते हैं और दूसरी ओर ईरान जैसे देशों से अपेक्षा करते हैं कि वे परमाणु हथियार न बनाएं। इस तरह के रवैए से हथियारों की होड़ नहीं रुकने वाली, बल्कि चुनौती और जरूरत के लिए हर देश परमाणु शक्ति संपन्न होना चाहेगा और परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ेगी ही।
पुरानी है विवाद की पटकथा
अरुण भगत, पूर्व प्रमुख, आईबी
देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की छवि इस हद तक दागदार हो जाएगी, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। संस्था के दो वरिष्ठतम अधिकारियों के बीच चल रहा विवाद नित नए रूप ले रहा है। इस सूरतेहाल में आने वाले दिनों के कयास संभव नहीं। मगर हां, इस पूरे घटनाक्रम ने देश के संजीदा लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। ऐसा हमने अक्सर देखा है कि किसी संस्था के शीर्ष स्तर के अधिकारियों या फैसले लेने वाले ओहदेदारों के बीच वैचारिक टकराव हुए हैं। लेकिन सीबीआई में अभी जिस तरह के मतभेद दिख रहे हैं, उसके उदाहरण शायद ही मिलते हैं। इस जांच एजेंसी के नंबर एक और नंबर दो के अधिकारी खुल्लमखुल्ला एक-दूसरे के खिलाफ मुखर हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक-दूसरे पर आपराधिक आरोप लगा रहे हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक-दूसरे के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज करा चुके हैं।
ऐसी नौबत आई क्यों? मेरा मानना है कि ऐसा अनदेखी की वजह से हुआ है। सीबीआई के हित में उचित समय पर उचित फैसला नहीं लिया गया। ऐसी चर्चाएं हैं कि इन दोनों अधिकारियों के बीच गंभीर मतभेद की पटकथा बहुत पहले तैयार हो चुकी थी। पिछले साल फरवरी में आलोक वर्मा को जब सीबीआई का निदेशक बनाया गया था, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही उन्हें अपने पूर्ववर्ती कार्यवाहक निदेशक (जो राकेश अस्थाना ही थे) के खिलाफ दो मामलों की जानकारी मिली थी। मगर तब आलोक वर्मा के लिए प्रतिकूल परिस्थिति यह थी कि उनके पास पहले कभी इस जांच एजेंसी में काम करने का कोई अनुभव नहीं था। इतना ही नहीं, उन्हें जब यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तब यह संस्था अपने दो पूर्व निदेशकों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार की जांच कर रही थी। इस कारण नए प्रमुख को सीबीआई की छवि को भी दुरुस्त करना था, जो इस जांच के कारण दागदार होने लगी थी।
रिपोर्ट ऐसी भी हैं कि आलोक वर्मा नहीं चाहते थे कि दागी छवि होने के कारण राकेश अस्थाना बतौर अतिरिक्त निदेशक विभाग में काम करते रहें। राकेश को यह पद दिसंबर, 2016 में दिया गया था। मगर जब अगस्त, 2017 में उन्हें प्रमोशन देकर विशेष निदेशक बनाने की बात हुई, तो कहा जा रहा है कि बतौर सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा ने मुख्य सतर्कता अधिकारी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर अस्थाना की जांच करने की मांग की थी और यह गुजारिश की थी कि उनको पदोन्नति न दी जाए। अगर यह घटनाक्रम सही है, तो यह वाकई आश्चर्य की बात है कि ‘निगेटिव नोट’ होने के बावजूद अस्थाना को भला कैसे प्रमोशन दिया गया? आखिर क्या वजह है कि उस वक्त उचित जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी नहीं किया गया? अगर तभी कुछ ठोस फैसला ले लिया गया होता, तो यूं आज सीबीआई की सार्वजनिक तौर पर इतनी छीछालेदार नहीं होती।
मेरा मानना है कि सीबीआई की विश्वसनीयता तब भी उतनी नहीं डिगी थी, जब उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ‘पिंजरे का तोता’ कहा था। ऐसा इसलिए, क्योंकि लोग यह मान चुके हैं कि देश में जिस किसी की भी सरकार बनती है, सीबीआई उसके हित में काम करती है। मगर हालिया घटनाक्रम अप्रत्याशित है। अब उन तमाम मामलों पर लोगों का संदेह बढ़ गया होगा, जिनकी जांच सीबीआई ने की है। कुछ मामलों की जांच में तो सीबीआई बिल्कुल विफल साबित हुई है।
दिलचस्प बात यह है कि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना, दोनों अधिकारियों के पास काम का लंबा अनुभव है। दोनों का अब तक का सर्विस रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। दोनों अधिकारियों पर किसी तरह के कोई दाग भी नहीं लगे थे। फिर भी, दोनों ‘एक्सट्रीम पोजिशन’ पर हैं, यानी दोनों का रुख अपने-अपने हिसाब से चरम पर है। ऐसा तब तक नहीं होता, जब तक कि मामला किसी दुस्साहसी मोड़ पर न आ गया हो। हालांकि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, उनसे तो यही लगता है कि यह आत्म-संरक्षण और नीतियों के बीच की जंग है, जिसमें आलोक वर्मा नीतियों की जंग लड़ रहे हैं, तो राकेश अस्थाना अपनी छवि बचाने में जुटे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम से सीबीआई की साख गिरी ही है, इससे उसका कामकाज भी प्रभावित हुआ होगा। इस संस्था के पास ढेरों काम हैं, पर पूरा का पूरा कुनबा अभी दो अधिकारियों का विवाद सुलझाने में जुटा होगा। चूंकि आमतौर पर सभी फाइलें सीबीआई प्रमुख तक पहुंचने से पहले विशेष निदेशक के टेबल से होकर गुजरती हैं, इसलिए इस आरोप-प्रत्यारोप का असर उन फाइलों पर भी निश्चित तौर पर पड़ रहा होगा। इसीलिए ताजा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने की जरूरत है। इसमें देरी इस संस्था की सेहत पर काफी भारी पड़ सकती है।
मौजूदा परिस्थिति में सबसे बड़ी चुनौती सीबीआई के पुराने गौरव को फिर से वापस पाने की है। यह काफी मुश्किल भरा काम है। इसमें वर्षों का समय लग सकता है। तमाम अधिकारियों और नीति-नियंताओं को इसके लिए संजीदगी दिखानी होगी। इस काम में उस अधिकारी की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होगी, जिन्हें अगले साल जनवरी में सीबीआई निदेशक का पद दिया जाना है। मेरा मानना है कि यह कुरसी ऐसे अधिकारी को मिलनी चाहिए, जिनके पास सीबीआई में काम करने का भी अनुभव हो। तब उनके पास संस्था के तमाम लोगों की अच्छाई और बुराई की जानकारी होगी। जरूरत उस ट्रेनिंग की फिर से समीक्षा करने की भी है, जो सीबीआई अधिकारियों को दी जाती है।
ताजा विवाद के बाद पूरी सीबीआई के ढांचे में बदलाव की जरूरत है। कानून अपना काम करेगा और ताजा विवाद में जिस किसी का भी दोष साबित होगा, उसे दंड मिलेगा। मगर सीबीआई की साख को बचाने के लिए ढांचागत बदलाव जरूरी है। इसके बिना हम इस दाग को शायद ही छुड़ा पाएं। हमें धैर्य के साथ काम करना होगा और नतीजे देने होंगे। संभव हो, तो ऐसी ‘एडवाइजरी बॉडी’ बनाई जाए, जो सीबीआई को सलाह दे। मामलों को उचित तरीके और बिना किसी दबाव के तेजी से निपटाना सीबीआई की प्राथमिकता होनी चाहिए।
Policy Paralysis
Government seems blind to the crisis in agriculture, slowdown in industry
Yoginder K. Alagh , [ The writer, an economist, is former Union minister]
This column hates to say we said so. Prices are not falling but the farmer is getting a rough deal. Industrial output and GDP growth is not picking up. It all comes out on the business page but the usual admonition that the economy will pick up is repeated by the senior-most officials from whom we actually expect answers to real problems. The terms of trade were doing badly for agriculture and the farmer was not doing too well. Big MSP increases without policy support, we argued, would not work and so it was. In the third week of October, news bureaus are reporting that mandi prices in bajra, maize, cotton and major oilseeds and pulses were ruling below support prices. Ten to 40 per cent deficiencies are common. It’s an avalanche, so the official stance is to say the rabi will be better! The claim that a 50 per cent increase in MSP has been provided over cost of production is not kosher any more on the field, apart from the criticism of many observers.
There is only token procurement in pulses and oilseeds because the prices the farmer has sown for are much higher and tariff policies are slow and don’t always help him because they are announced after the imports have taken place. The government hardly ever imposes a high enough tariff because of the needs of the consumer and so the fight goes on. When prices are rising this is a tough policy bind. Balancing farmer interests and fighting inflation needs the kind of strategic thinking that is not seen much apart from by the central bank. NAFED does some procurement but it is usually short of funds. The real issue of markets, first-stage processing and supply chains, lies elsewhere. As an example, getting Walmart to buy farmers produce and give them space in its warehouses is far more important as an alternative supply channel. But we are also told that its case is slowed down because of powerful lobbies.
Prices are simultaneously rising for the consumer. Policymakers took credit for retail inflation falling from 4.85 per cent in July to 3.69 per cent in August but it was left to Cassandras like me to say that last year it was 3.28 per cent and there is seasonality in food prices. It was 3.7 per cent in September but now the wholesale price index rising year-on-year to 5.13 per cent demands a policy response, before the wage price agitations start in a pre-election year. In the third week of October, a former governor of the RBI gives us great comfort by complimenting economic policy and also sagely advising that the continuation of a strong central government next year will be good, but another not-so-savvy governor, Y V Reddy, has warned of the pitfalls ahead.
The turnaround for the worse in industrial output is the most distressing. It was chugging along merrily and clocked 6 per cent in July with a rate of 5.4 per cent growth in the period March to July this year. We were quite optimistic and this column took the position that now is the time to consolidate, push up investment which was lagging and ensure a good year ahead. But the index of industrial production, that terrible mirror face of industrial output, went down to a low of 4.35 in August. This is a setback.
It would be good if policy-making took this as a temporary hiccup and got back to the drawing board on giving industrial output the stimulus it needs. It may be said that in a pre-election year, this is a tall order requiring as it does some tough resource raising decisions. But then, if the economy responds with a four-month lag, which should be expected from most policy models, higher industrial output and employment will again underline that good economics is also good politics. Meanwhile, will somebody in authority at least talk of the real problem?
Trouble at the top
Firm intervention is needed to end the unsavoury controversy in the CBI
EDITORIAL
At one level, what is going on in the Central Bureau of Investigation (CBI) is a ‘turf war’, a battle of egos between two individuals at the helm. But the unsavoury developments involving the CBI Director and its Special Director are reflective of a much deeper malaise — a big rot at the very heart of the premier investigating agency. That the CBI registered a First Information Report against its own Special Director is extraordinary. The most troubling aspect of the ongoing crisis involving Director Alok Verma and Special Director Rakesh Asthana is that only one of them will be proved right; either way, it is the agency that will be shown in a poor light. If the Director is justified in embarking on a high-profile probe into bribery charges against Mr. Asthana, it can only mean that corruption is so pervasive that even the second-in-command in the agency is not beyond demanding ₹3 crore to let someone off the hook. On the other hand, if Mr. Asthana is shown to be wrongly implicated, and his own charges — set out in a complaint to the Central Vigilance Commission — that other CBI officers are interfering in ongoing probes are proved right, the situation will be no better. It cannot be forgotten that this controversy was preceded only recently with two Directors of the CBI coming under a cloud. The Supreme Court held that the charges that Ranjit Sinha, when heading the agency, sought to help the accused in several cases and interfered in ongoing probes were ‘prima facie credible’; as a result, he was asked to keep away from the 2G telecom cases. Similarly, A.P. Singh, another director, was booked last year for alleged links with meat exporter Moin Qureshi. Clearly, the existing procedure for the appointment of CBI Directors, which is made by a committee comprising the Prime Minister, the Chief Justice of India and the Leader of the Opposition, has not stripped the office of controversy.
And now as well, it is the Qureshi case that continues to haunt the agency. Its investigating officer, a Deputy Superintendent of Police, has been arrested on the charge of fabricating a statement by a Hyderabad-based businessman “to corroborate baseless charges” made by Mr. Asthana against Mr. Verma in a complaint to the CVC. The CBI labours under a dual image: an independent agency in the perception of those disillusioned with the conduct of the jurisdiction police, and a ‘caged parrot’ or a handmaiden of the ruling party at the Centre in the eyes of the national Opposition. Recent developments, in which Central agencies are seen as targeting those in Opposition parties, add to the latter perception and do not augur well for its credibility. To a large extent, the political leadership must bear the primary responsibility for such controversies. It is difficult to ignore the fact that Mr. Asthana’s appointment as Special Director was made despite Mr. Verma’s vehement objections about his suitability, something the CVC chose to overrule. In such circumstances, it is up to the CVC and the Centre to address the present crisis. A good place to start will be to take Mr. Asthana, whose name already figures in a case, temporarily out of the agency to ensure an impartial probe.