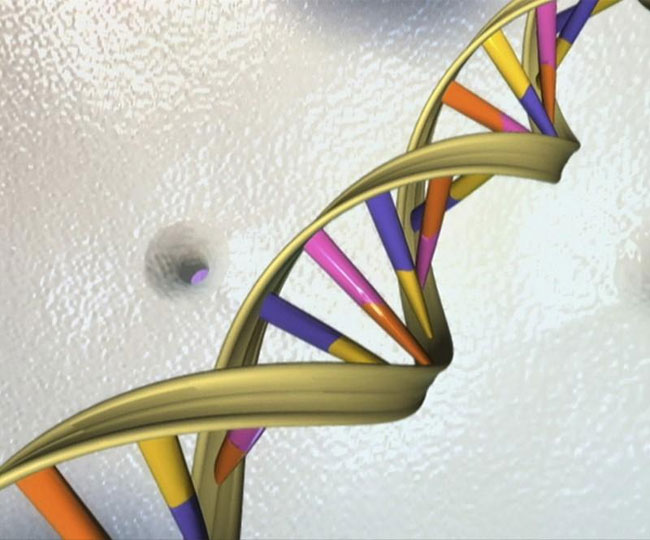24-02-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Walk the talk on praise for Nari Shakti
ET Editorial
Prime Minister Modi loses no opportunity to promote nari shakti or women power.His Beti Bachao Beti padhao campaign (save and tech daughters) has arguably contributed to the decline of female foeticide in some parts of haryana.in his latest radio broadcast, the PM commended a young girl who is on mission to climb the tallest peal on every continent.Yet there is a gap between what the pm says and what his government,his political supporters and religious conservatives profess.
The goverment opposed combat roles for women soldiers,only to be overruled by the supreme court.the head of the rashtriya swayamsevak sangh,the ruling party’s ideological parent, spoke against divorce,seeming to suggest that education of women was responsible for such sources of social instability,oblivious to the reality that most divorces occur when women find the agency to walk out of oppressive marriages.in a Gujarat college run by a religious group,young women were strip-searched for signs of menstruation:the colleges rules enforce an age-old custom of isolating menstrual women.such incidents are over and above the daily barrage of news about sexual assaults on women, honor killings,gender pay-gaps and bulletproof glass ceilings.Democracy is not just about voting in a set of leaders once every five year. It is about removing iniquitous power imbalances in society, including those between men and women. Political leaders of every persuasion should as part of deepening Indian democracy,strive to empower women.
The PM in particular, is well placed to play a weighty role in this process,given the enormous political capital he has accumulated.We urge him to clout to take on conservative prejudices against women, regardless of the source of the prejudice.
टाले जाएं डेटा सर्वेक्षण
संपादकीय
भारत विभिन्न स्तरों पर डेटा गुणवत्ता की समस्या का सामना करता है और इन आंकड़ों के अक्सर देर से आने से समुचित नीतिगत कदम उठाने में विलंब होता है। विश्वसनीय आर्थिक सांख्यिकी की समस्या अब अधिक गंभीर होने की आशंका है। अभी तक यह समस्या महज सरकार की स्वीकृति और सर्वे के परिणाम जारी करने तक ही सीमित थी लेकिन अब यह वहां तक पहुंच चुकी है जहां खुद डेटा संग्रह ही एक समस्या बनती जा रही है। इस समाचारपत्र में पिछले हफ्ते प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण टालना पड़ सकता है क्योंकि लोग इन सर्वेक्षणों के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें डर यह है कि सरकार इस जानकारी का इस्तेमाल नागरिकता-निर्धारण के लिए कर सकती है। नतीजतन, एक विशेषज्ञ समिति ने यह सुझाव देने का फैसला किया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा घरेलू पर्यटन व्यय एवं अन्य संकेतकों के सर्वेक्षण का काम टाल दिया जाए। निश्चित रूप से सरकार के पास यह विकल्प है कि वह यह सलाह न माने। लेकिन इससे दो बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
पहली, परिवारों की समुचित भागीदारी न होने से सर्वे की अपेक्षित गुणवत्ता नहीं रह जाएगी जिससे इसका उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। दूसरी, यह उस जगह पर सर्वेक्षकों की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकता है जहां आबादी का एक बड़ा तबका नागरिकता प्रावधानों को लेकर परेशान है। कई राज्यों में सर्वे करने गए फील्ड अफसरों पर हमले की घटनाएं देखी गई हैं। मसलन, पश्चिम बंगाल में आर्थिक जनगणना और समय-समय पर होने वालेे श्रमिक बल सर्वेक्षण रोक दिए जाने की खबरें हैं। इससे भी बुरा यह है कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति न केवल इस समय जारी सर्वेक्षणों को प्रभावित कर रही है बल्कि आगामी जनगणना को भी खतरे में डाल सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका निहितार्थ अधिक व्यापक होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली समेत अलग-अलग हिस्सों में अब भी जारी हैं।
कई राज्य सरकारों ने यह घोषणा की है कि वे सीएए को लागू नहीं करेंगी और वे राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी को अद्यतन करने के भी पक्ष में नहीं हैं। लोगों के बीच अविश्वास बढऩे और केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच मतभेद से जनगणना की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। देश के पूर्व मुख्य सांख्यिकी अधिकारी प्रणव सेन ने गत दिनों इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि अगर जनगणना का काम सही ढंग से नहीं किया जाता है तो अगले 10 वर्षों तक होने वाले सारे घरेलू सर्वेक्षण भरोसेमंद नहीं रहेंगे क्योंकि ये जनगणना ढांचे पर ही आधारित रहे हैं। इस तरह डेटा की विश्वसनीयता पर आगे और भी सवाल उठेंगे। इससे न केवल नीति-निर्माण प्रभावित होगा बल्कि यह पहले से ही संदेह में घिरी सांख्यिकीय प्रणाली की समग्र विश्वसनीयता को भी चोट पहुंचाएगा। मसलन, जीडीपी से जुड़े आंकड़े पर कई अर्थशास्त्री सवाल उठा चुके हैं। रोजगार संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन टालने और उपभोग सर्वेक्षण बंद करने के सरकार के फैसलों ने भी हालत कमजोर की है। हालांकि मौजूदा समस्या कहीं अधिक बड़ी है और अगर सरकार जरूरी कदम उठाती है तो वह बेहतर होगा।
डेटा सर्वेक्षणों को लेकर विश्वसनीयता पैदा करने का दायित्व केंद्र सरकार का है क्योंकि यह समस्या नागरिकता कानून में बदलावों से शुरू हुई है। भारत एक खंडित सांख्यिकीय प्रणाली के साथ आगे बढऩे की हालत में नहीं होगा। अगर असमंजस को जल्द दूर नहीं किया जाता है तो भारत की भी गिनती उन देशों में होने लगेगी जो अपनी आर्थिक स्थिति को वास्तविकता से बेहतर दिखाने के लिए आंकड़ों में फेरबदल करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारी सांख्यिकीय प्रणाली में बड़ी समस्याएं हैं और उन्हें दूर करने की जरूरत है। सरकार के लिए यह वक्त नीति को राजनीति के ऊपर रखने का है।
संघर्षों से निकले, देश को पेटेंट के लिए लड़ना सिखाया
डॉ. रघुनाथ मालेशकर, (वरिष्ठ वैज्ञानिक, लेखक और संगठनकर्ता)
मैं खासतौर पर बताना चाहूंगा कि हमारी हल्दी, नीम और बासमती चावल को अमेरिका ने अपने नाम पेटेंट करा रखा था। मैंने विश्व स्तर पर इसके खिलाफ 14 महीने तक लड़ाई लड़कर इसे भारत के नाम कराया और जनरल इलेक्ट्रिक (GE) जैसे विश्व स्तरीय संगठन में हम शामिल हो गए। इससे GE ने बेंगलुरु में एक रिसर्च सेंटर स्थापित कर दिया। इस दौरान मेरे थोड़े से प्रयासों से देश ने लगातार पेटेंट हासिल किए जिससे अमेरिका व यूरोप में हमारी धाक जमने लगी। मेरे मार्गदर्शन में हर विषय से संबंधित भारत के पारंपरिक ज्ञान-विज्ञान के तीन करोड़ दस्तावेज संग्रहीत कर उनकी ई-लाइब्रेरी बनाई गई। यह डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि हमारा प्राचीन विज्ञान पन्नों के साथ ही नष्ट न हो जाए। इसी के साथ पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक प्रणालियों से जोड़कर नए प्रयोग की शुरुआत हुई। 1991 में पद्मश्री और 2000 में पद्मभूषण पुरस्कार मिल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी ‘स्टार्स ऑफ एशिया’अवार्ड प्रदान किया। मेरी कुछ उपलब्धियां जैसे- सुपरकंडक्टिविटी, हरित क्रांति, परमाणु ऊर्जा, आधुनिक चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान का संयोजन, अतिचालकता, सीएसआईआर के परिवर्तन की स्वर्ण त्रिभुज अवधारणा को जोड़ना तथा पंचशीलता का सिद्धांत हैं। आने वाले समय में स्पर्धा उत्पादकों में नहीं, बल्कि कौशल्य आधारित होगी। आपकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि आप किन कौशलों का साथ में उपयोग करते हैं।
जीवन में बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। इंग्लैंड, फ्रांस जर्मनी, अमेरिका सहित विश्व के 25 महाविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी, लेकिन इन सब के पीछे मैं मां को देखता हूं। मेरी पहली गुरु, मेरी पहली यूनिवर्सिटी मां थीं, उन्होंने जीवन मूल्य और मुसीबत से कैसे निकला जाए यह सिखाया। मेरा मानना है कि पूरे समाज की उन्नति में फाइव-ई महत्वपूर्ण होता है- एन्वायर्नमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इक्वेलिटी और एथिक्स। ज्ञान के माध्यम से ही धन का सृजन होना चाहिए। रिसर्च, पैसे को ज्ञान में बदल सकती है, लेकिन इनोवेशन, ज्ञान को पैसे में बदल देता है।
जैसे विश्व स्तरीय संगठन में हम शामिल हो गए। इससे GE ने बेंगलुरु में एक रिसर्च सेंटर स्थापित कर दिया। इस दौरान मेरे थोड़े से प्रयासों से देश ने लगातार पेटेंट हासिल किए जिससे अमेरिका व यूरोप में हमारी धाक जमने लगी। मेरे मार्गदर्शन में हर विषय से संबंधित भारत के पारंपरिक ज्ञान-विज्ञान के तीन करोड़ दस्तावेज संग्रहीत कर उनकी ई-लाइब्रेरी बनाई गई। यह डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि हमारा प्राचीन विज्ञान पन्नों के साथ ही नष्ट न हो जाए। इसी के साथ पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक प्रणालियों से जोड़कर नए प्रयोग की शुरुआत हुई। 1991 में पद्मश्री और 2000 में पद्मभूषण पुरस्कार मिल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी ‘स्टार्स ऑफ एशिया’ अवॉर्ड प्रदान किया। मेरी कुछ उपलब्धियां जैसे- सुपरकंडक्टिविटी, हरित क्रांति, परमाणु ऊर्जा, आधुनिक चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान का संयोजन, अतिचालकता, सीएसआईआर के परिवर्तन की स्वर्ण
लंदन में पढ़ाई के दौरान कॅरियर बनाने के लिए कई देशों से आमंत्रण मिले थे, लेकिन मैंने स्वदेश लौटना पसंद किया। पहली नौकरी 1976 में 2100 रुपए महीने से शुरू की। मेरा काम और लगन देखकर 1989 में मुझे एनसीएल निदेशक, पुणे की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मैंने औद्योगिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च किए और कम समय में एक नया मॉडल स्थापित कर दिया। लगातार कुछ नया करते रहने से 1995 में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) का महासंचालक बना दिया गया। यहां मैंने 11 वर्ष तक सेवाएं देते हुए देशभर की सभी प्रयोगशालाओं का नेतृत्व किया और अनुसंधान के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए। मैंने जमीनी स्तर पर प्रयोग करने वालों को हर संभव आगे बढ़ाने की कोशिश की। पहली बार विचार आया कि हमारा शोध कानूनन पेटेंट होना चाहिए, क्योंकि 1950 से 39 वर्षों में हमारा कोई पेटेंट नहीं था।
मैं खासतौर पर बताना चाहूंगा कि हमारी हल्दी, नीम और बासमती चावल को अमेरिका ने अपने नाम पेटेंट करा रखा था। मैंने विश्व स्तर पर इसके खिलाफ 14 महीने तक लड़ाई लड़कर इसे भारत के नाम कराया और जनरल इलेक्ट्रिक (GE) जैसे विश्व स्तरीय संगठन में हम शामिल हो गए। इससे GE ने बेंगलुरु में एक रिसर्च सेंटर स्थापित कर दिया। इस दौरान मेरे थोड़े से प्रयासों से देश ने लगातार पेटेंट हासिल किए जिससे अमेरिका व यूरोप में हमारी धाक जमने लगी। मेरे मार्गदर्शन में हर विषय से संबंधित भारत के पारंपरिक ज्ञान-विज्ञान के तीन करोड़ दस्तावेज संग्रहीत कर उनकी ई-लाइब्रेरी बनाई गई। यह डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि हमारा प्राचीन विज्ञान पन्नों के साथ ही नष्ट न हो जाए। इसी के साथ पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक प्रणालियों से जोड़कर नए प्रयोग की शुरुआत हुई। 1991 में पद्मश्री और 2000 में पद्मभूषण पुरस्कार मिल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी ‘स्टार्स ऑफ एशिया’ अवॉर्ड प्रदान किया। मेरी कुछ उपलब्धियां जैसे- सुपरकंडक्टिविटी, हरित क्रांति, परमाणु ऊर्जा, आधुनिक चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान का संयोजन, अतिचालकता, सीएसआईआर के परिवर्तन की स्वर्ण त्रिभुज अवधारणा को जोड़ना तथा पंचशीलता का सिद्धांत हैं। आने वाले समय में स्पर्धा उत्पादकों में नहीं, बल्कि कौशल्य आधारित होगी। आपकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि आप किन कौशलों का साथ में उपयोग करते हैं।
लेखन और अभिनय में भी मेरी खास रुचि थी (यही कारण है कि अनेक पुस्तकें लिख चुका हूं)। इतने अभावों में पढ़ने के बावजूद बोर्ड परीक्षा में महाराष्ट्र में मैंने 11वां स्थान हासिल किया। अब आगे पढ़ने के पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कुछ समय पढ़ाई बंद कर कोई काम कर लेता हूं, लेकिन मां ने मना किया। वे बोलीं कि आप पढ़ने में अव्वल हैं, स्कॉलरशिप मिल जाए, ऐसा कुछ करो। मैंने जानकारी निकाली और ‘सर दोराबजी टाटा स्कॉलरशिप’ परीक्षा पास करने में जी-जान लगा दिया। नतीजा, जयहिंद कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश मिल गया। यहीं से मैंने अव्वल नंबर से पीएचडी पूरी की तो लंदन की सेलफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छात्रवृत्ति देकर अपने यहां दाखिला दे दिया। जब हम अव्वल नंबर आते हैं तो दुनिया आपको हाथोंहाथ उठा लेती है। इस तरह झोपड़ी से निकलकर मैं लंदन में पढ़ने चला गया। एक दिन नेशनल केमिकल लेबोरेटरी (एनसीएल) के तत्कालीन संचालक डॉ. बी.डी तिलक ने सूचना भेजी कि तुरंत सीएसआईआर (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) के महासंचालक डॉ. नायुदम्मा से मिलो। आगे की रिसर्च उन्हीं के मार्गदर्शन में करने लगा।
लंदन में पढ़ाई के दौरान कॅरियर बनाने के लिए कई देशों से आमंत्रण मिले थे, लेकिन मैंने स्वदेश लौटना पसंद किया। पहली नौकरी 1976 में 2100 रुपए महीने से शुरू की। मेरा काम और लगन देखकर 1989 में मुझे एनसीएल निदेशक, पुणे की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मैंने औद्योगिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च किए और कम समय में एक नया मॉडल स्थापित कर दिया। लगातार कुछ नया करते रहने से 1995 में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) का महासंचालक बना दिया गया। यहां मैंने 11 वर्ष तक सेवाएं देते हुए देशभर की सभी प्रयोगशालाओं का नेतृत्व किया और अनुसंधान के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए। मैंने जमीनी स्तर पर प्रयोग करने वालों को हर संभव आगे बढ़ाने की कोशिश की। पहली बार विचार आया कि हमारा शोध कानूनन पेटेंट होना चाहिए, क्योंकि 1950 से 39 वर्षों में हमारा कोई पेटेंट नहीं था।
मेरा जन्म गोवा के माशेल गांव में 1 जनवरी 1943 को एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। जब छह वर्ष का था तभी पिता चल बसे। रोजीरोटी के लिए मां अंजनीबाई मुझे लेकर मुंबई के गिरगांव आ गईं। वहीं के म्यूनिसिपल स्कूल में दाखिला लिया। मजदूरी के साथ-साथ घरों में जो काम मिल जाता था, मां कर लेती थीं, फिर भी दो वक्त का भोजन हमें नसीब नहीं होता था। गरीबी ऐसी थी कि 12 वर्ष का होने तक मुझे चप्पल पहनने को नहीं मिली। यह वह समय था जब मजदूरी भी कुछ सिक्कों में मिलती थी। सातवीं कक्षा में प्रवेश फीस के लिए 21 रुपए भी नहीं थे। पढ़ाई के प्रति मेरा जुनून मां को पता था, इसलिए उन्होंने एक कामवाली बाई से 21 रुपए उधार लिए। उस समय 21 रुपए बहुत मायने रखते थे। गणित और विज्ञान विषय में मेरी विशेष रुचि थी। पागलपन की हद तक पढ़ना चाहता था, लेकिन पुस्तकें खरीद नहीं सकता था। इसलिए घंटों पुस्तकालय में बैठकर पढ़ाई करता रहता था। इसके बाद आधी रात तक स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था।
लेखन और अभिनय में भी मेरी खास रुचि थी (यही कारण है कि अनेक पुस्तकें लिख चुका हूं)। इतने अभावों में पढ़ने के बावजूद बोर्ड परीक्षा में महाराष्ट्र में मैंने 11वां स्थान हासिल किया। अब आगे पढ़ने के पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कुछ समय पढ़ाई बंद कर कोई काम कर लेता हूं, लेकिन मां ने मना किया। वे बोलीं कि आप पढ़ने में अव्वल हैं, स्कॉलरशिप मिल जाए, ऐसा कुछ करो। मैंने जानकारी निकाली और ‘सर दोराबजी टाटा स्कॉलरशिप’ परीक्षा पास करने में जी-जान लगा दिया। नतीजा, जयहिंद कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश मिल गया। यहीं से मैंने अव्वल नंबर से पीएचडी पूरी की तो लंदन की सेलफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छात्रवृत्ति देकर अपने यहां दाखिला दे दिया। जब हम अव्वल नंबर आते हैं तो दुनिया आपको हाथोंहाथ उठा लेती है। इस तरह झोपड़ी से निकलकर मैं लंदन में पढ़ने चला गया। एक दिन नेशनल केमिकल लेबोरेटरी (एनसीएल) के तत्कालीन संचालक डॉ. बी.डी तिलक ने सूचना भेजी कि तुरंत सीएसआईआर (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) के महासंचालक डॉ. नायुदम्मा से मिलो। आगे की रिसर्च उन्हीं के मार्गदर्शन में करने लगा।
मेरा जन्म गोवा के माशेल गांव में 1 जनवरी 1943 को एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। जब छह वर्ष का था तभी पिता चल बसे। रोजीरोटी के लिए मां अंजनीबाई मुझे लेकर मुंबई के गिरगांव आ गईं। वहीं के म्यूनिसिपल स्कूल में दाखिला लिया। मजदूरी के साथ-साथ घरों में जो काम मिल जाता था, मां कर लेती थीं, फिर भी दो वक्त का भोजन हमें नसीब नहीं होता था। गरीबी ऐसी थी कि 12 वर्ष का होने तक मुझे चप्पल पहनने को नहीं मिली।
मूल समस्या की अनदेखी करते ट्रंप
भरत झुनझुनवाला, (लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग है कि भारत के बाजार को चिकन, चीज आदि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोला जाए जिससे कि अमेरिकी किसानों को लाभ हो, परंतु भारत इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे हमारे किसानों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस समय अमेरिका और भारत एक व्यापक व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी रणनीति तय करनी होगी, लेकिन इसके लिए समझना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत को अमेरिकी निर्यात क्यों बढ़ाना चाहते हैं।
दरअसल अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूर्व में नए-नए तकनीकी विकासों के आधार पर आगे बढ़ रही थी। जैसे अमेरिका में ही परमाणु रिएक्टर, जेट हवाई जहाज, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का आविष्कार हुआ था। इन हाईटेक मालों का निर्यात करके अमेरिका भारी लाभ कमा रहा था। इस लाभ से वह अपनी जनता को ऊंचे वेतन दे रहा था, लेकिन बीते दो दशकों में अमेरिका में ऐसे कोई आविष्कार नहीं हुए हैं, जिसका निर्यात कर वह भारी लाभ कमा सके। इस कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी हुई है, श्रमिकों के वेतन दबाव में हैं और अमेरिकी सरकार को टैक्स कम मिल रहा है, लेकिन अमेरिकी सरकार के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं।
जैसे उसे अफगानिस्तान और ईरान से युद्ध करने के लिए खर्च करने पड़े हैं। इस बजट घाटे को पाटने के लिए सरकार बांड बेच रही है और ऋण ले रही है। इस ऋण का बड़ा हिस्सा विदेशों से आ रहा है विशेषकर चीन एवं जापान से। इस कारण अमेरिकी डॉलर का दाम बढ़ रहा है। जैसे चीन के निवेशक ने 100 डॉलर के अमेरिकी सरकार के बांड खरीदे तो बाजार में डॉलर की मांग बढ़ी। मांग बढ़ने से डॉलर के दाम बढ़ गए। इस विदेशी पूंजी के आवक से डॉलर के मूल्य ऊंचे बने हुए हैं और अमेरिका कृत्रिम अमीरी का आनंद ले रहा है।
डॉलर के ऊंचा होने का सीधा प्रभाव अमेरिका के विदेश व्यापार पर पड़ रहा है। डॉलर महंगा होता है तो अमेरिका में माल का आयात अधिक होता है। जैसे मान लीजिए भारत में एक ग्लेडियोलस फूल के उत्पादन का मूल्य 15 रुपये पड़ता है। यदि एक डॉलर का मूल्य 15 भारतीय रुपये हो, जैसा कि आज से 30 वर्ष पूर्व था तो अमेरिकी उपभोक्ता को एक डॉलर में एक ग्लेडियोलस फूल मिलेगा, लेकिन यदि एक डॉलर का मूल्य 75 रुपये हो, जैसा कि आज है तो उसी एक डॉलर में अमेरिकी उपभोक्ता को पांच ग्लेडियोलस के फूल मिलेंगे। जाहिर है अमेरिकी डॉलर का मूल्य ऊंचा होने से अमेरिका में भारी मात्रा में आयात हो रहे हैं और निर्यात दबाव में हैं।
इसलिए अमेरिकी सरकार के खर्च अधिक होने से, बजट घाटा बढ़ने से, ऋण ज्यादा लेने से, विदेशी पूंजी के आने से और डॉलर का मूल्य ऊंचा होने से अमेरिका के आयात बढ़ रहे हैं, निर्यात दबाव में हैं और व्यापार घाटा बढ़ रहा है। अमेरिका के व्यापार घाटे के बढ़ने का रहस्य बजट घाटे के बढ़ने में है। राष्ट्रपति ट्रंप व्यापार घाटे से चिंतित हैं। उन्हें अपना बजट घाटा नहीं दिख रहा है। इसलिए उन्होंने भारत से आयातित स्टील पर आयत कर बढ़ाए हैं। अपने व्यापार घाटे को नियंत्रण करने के लिए वे चाहते हैं कि भारत अमेरिकी माल का आयात बढ़ाए।
लेकिन ट्रंप अपने उद्देश्य को हासिल करने में निश्चित रूप से असफल होंगे। अमेरिकी सरकार के बजट घाटे के बने रहने से और विदेशी पूंजी के प्रवेश करने से व्यापार घाटा कम हो ही नहीं सकता है। इसे ऐसे समझिए, किसी परिवार की आय कम है, वह लगातार ऋण ले रहा है और शोर मचा रहा है कि दुकानदार ने कपड़े का अनुचित दाम वसूला है। मूल विषय तो परिवार की आय का है। जब आय ही नहीं है तो यदि दुकानदार ने कपड़े का दाम कम भी कर दिया तो परिवार आटे- दाल के ऊंचे दाम पर शोर मचाएगा। ऐसा शोर करने से परिवार की आय नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार जब तक अमेरिकी सरकार का बजट घाटा बना रहेगा तब तक अमेरिकी सरकार का व्यापार घाटा कम हो ही नहीं सकता है।
इस परिस्थिति में राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी माल के आयात बढ़ाए। उन्होंने भारत के स्टील उत्पादों पर आयात कर बढ़ा दिए हैं। इन कदमों से अमेरिका की समस्या हल नहीं होगी। यदि भारत अमेरिका के माल को प्रवेश करने भी देता है तो वही व्यापार घाटा किसी दूसरे देश को स्थानांतरित हो जाएगा। जैसे वियतनाम और फिलीपींस से आयात बढ़ जाएंगे। व्यापार घाटे के बढ़ने का जो वास्तविक कारण है वह पूर्ववत बना ही रहेगा। अपने बजट घाटे पर नियंत्रण करने के स्थान पर ट्रंप बेवजह ही भारत पर दोष लगा रहे हैं।
वास्तव में राष्ट्रपति ट्रंप का उद्देश्य अपनी घरेलू राजनीति को साधना है। वे अपनी जनता को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने दूसरे देशों के ऊपर सख्ती की है और अमेरिकी हितों को हासिल किया है। वे इस बात को अपनी जनता को नहीं बताना चाहते कि उनकी सरकार का बजट घाटा समस्या की जड़ है। इस परिस्थिति में हमें अपने हितों की रक्षा करनी है।
राष्ट्रपति ट्रंप का दबाव है कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात के लिए अपने बाजार खोले। अब भारत इसके खिलाफ अड़ा रह सकता है अथवा इसके बदले में अमेरिका से कुछ मांग सकता है। जैसे कि भारत अपने स्टील के निर्यातों को बढ़ा सकता है, नई तकनीकों को हासिल कर सकता है अथवा अपने सेवा क्षेत्र के निर्यातों के लिए अमेरिकी बाजार को खोलने के लिए कह सकता है। हमें तय करना है कि हम अपने किस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे।
मेरा मानना है कि संपूर्ण विश्व की तरह भारत में भी कृषि का ह्रास तो होगा ही। इस समय जरूरत है कि हम सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दें जिससे हम अपने युवाओं को रोजगार दे सकें। हम चिकन और चीज का आयात होने दे सकते हैं। इससे अपने किसानों को होने वाली हानि को हमें बर्दाश्त करना ही होगा। इसके बदले में अमेरिका से अपनी सेवाओं के निर्यात को सुलभ बनाने का रास्ता मांगना चाहिए। इस प्रकार के लेन-देन से राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी घरेलू राजनीति में लाभ होगा। वे अपने नागरिकों से कह सकेंगे कि उन्होंने भारत को कृषि के सूर्यास्त क्षेत्र में चित कर दिया है, लेकिन हम अपने सूर्योदय सेवा क्षेत्र के निर्यात से उनके बाजार में प्रवेश करेंगे और उन्हें ही चित कर सकेंगे।
जीनोम मेपिंग – सेहत की नई क्रांति
प्रदीप, (विज्ञान विषय के जानकार)
हाल ही में विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय ने एक परियोजना के तहत जैव-प्रौद्योगिकी विभाग को भारत के बीस हजार लोगों के जीनोम की सिक्वेंसिंग यानी अनुक्रमण किए जाने की योजना को मंजूरी दी है। यह पहला मौका होगा जब भारत में इतने बड़े स्तर पर जीनोम के गहन अध्ययन के लिए खून के नमूने एकत्रित किए जाएंगे। इसके लिए ‘जीनोम इंडिया’ प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है। 240 करोड़ लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत की आनुवंशिक विविधता के निर्धारण की दिशा में पहला प्रयास माना जा रहा है।
हम जीव विज्ञान की सदी में रह रहे हैं। अगर 20वीं सदी भौतिक विज्ञान की सदी थी तो 21वीं सदी जैव-प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की होगी। पिछले दो-तीन दशकों में जैव-प्रौद्योगिकी में, विशेषकर आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कृत कर देने वाले नए अनुसंधान तेजी से बढ़े हैं। ऐसा स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, उद्योग आदि क्षेत्रों में, जिनके केंद्र बिंदु में जीव जगत है, के सतत मांग की वजह से मुमकिन हुआ है।
मात्र दो अक्षरों का शब्द ‘जीन’ आज मानव इतिहास की दशा और दिशा बदलने में समर्थ है। जीन सजीवों में सूचना की बुनियादी इकाई और डीएनए का एक हिस्सा होता है। जीन इस लिहाज से स्वार्थी होते हैं कि उनका एकमात्र उद्देश्य होता है स्वयं की ज्यादा से ज्यादा प्रतिलिपियों को अगली पीढ़ी में पहुंचाना। इसलिए जीन माता-पिता व पूर्वजों के गुण और रूप-रंग संतान में पहुंचाता है। कह सकते हैं कि काफी हद तक हम वैसा ही दिखते हैं या वही करते हैं, जो हमारे शरीर में छिपे सूक्ष्म जीन तय करते हैं। डीएनए के उलट-पुलट जाने से जींस में विकार पैदा होता है और इससे आनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो पीढ़ी-दर- पीढ़ी बच्चों को अपने पुरखों से विरासत में मिलती हैं।
मानव शरीर में जीनों की संख्या अस्सी हजार से एक लाख तक होती है। इस विशाल समूह को ‘जीनोम’ नाम से जाना जाता है। जीनोम के अध्ययन को जीनोमिक्स कहा जाता है। चूंकि शरीर में क्रियाशील जीन की स्थिति ही बीमारी विशेष को आमंत्रित करती है, इसलिए वैज्ञानिक लंबे समय से मनुष्य की जीन कुंडली को पढ़ने में जुटे हैं। 1988 में अमेरिकी सरकार ने अपनी ‘ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट’ की शुरुआत की। मानव आनुवंशिकी और जीनोम विश्लेषण पर इस सबसे बड़ी परियोजना को वर्ष 2003 में पूरा किया गया। वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट के जरिये इंसान के पूरे जीनोम को पढ़ा। इस परियोजना का लक्ष्य जीनोम सिक्वेंसिंग के जरिये बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने, दवाओं के शरीर पर प्रभाव की सटीक भविष्यवाणी, फोरेंसिक विज्ञान में उन्नति और मानव विकास को समझने में मदद हासिल करना था।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बीस हजार लोगों के जीनोम की सिक्वेंसिंग किए जाने की योजना ने जीनोमिक्स के क्षेत्र में भारत के प्रवेश की भूमिका तैयार कर दी है जिससे चिकित्सा विज्ञान में नई संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। इस परियोजना में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान एवं कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित लगभग 20 संस्थान शामिल होंगे। जीनोम की सिक्वेंसिंग खून के नमूने के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में मौजूद एडानीन, गुआनीन, साइटोसीन और थायमीन के सटीक क्रम का पता लगाया जाएगा।
डीएनए सीक्वेंसिंग से लोगों की बीमारियों का पता लगाकर समय रहते इलाज किया जा सकता है। साथ ही भावी पीढ़ी को रोगमुक्त करना संभव होगा। परियोजना में भाग लेनेवाले छात्रों को बताया जाएगा कि क्या उनमें जीन वेरिएंट हैं जो उन्हें कुछ दवाओं के प्रति कम संवेदनशील बनाते हैं। दुनिया के कई देश अब अपने नागरिकों की जीनोम मैपिंग करके उनके यूनीक जेनेटिक ट्रेट्स को समझने में लगे हैं, ताकि किसी बीमारी विशेष के प्रति उनकी संवेदनशीलता के मद्देनजर व्यक्तिगत दवाओं को तैयार करने में मदद मिल सके।
मानव जीनोम को अनुक्रमित किए जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय आनुवंशिक संरचना तथा रोग के बीच संबंध को लेकर वैज्ञानिकों को एक नई संभावना दिख रही है। जीनोम अनुक्रम को जान लेने से यह पता लग जाएगा कि कुछ लोग कैंसर, कुछ मधुमेह और अल्जाइमर और अन्य बीमारियों से ग्रस्त क्यों होते हैं। हम यह जान सकते हैं कि किसको कौन सी बीमारी हो सकती है और उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। जीनोम मैपिंग से बीमारी होने का इंतजार किए बगैर व्यक्ति की जीन-कुंडली को देखते हुए उसका इलाज पहले से शुरू किया जा सकेगा। इसके माध्यम से पहले से ही पता लगाया जा सकेगा कि भविष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है। वह बीमारी न होने पाए तथा इसके नुकसान से कैसे बचा जाए इसकी तैयारी आज से ही शुरू की जा सकती है।
लगभग दस हजार बीमारियां हैं जिनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया शामिल हैं, जिनके होने का कारण एकल जीन में खराबी को माना जाता है। जीनोम थेरैपी के जरिये दोषपूर्ण जीन को निकाल कर स्वस्थ जीन को रोपित करना संभव हो सकेगा। अब समय आ गया है कि भारत अपनी खुद की जीनोमिक्स क्रंति की शुरुआत करे। तकनीकी समझ और इसे सफलतापूर्वक लॉन्च करने की क्षमता हमारे देश के वैज्ञानिकों तथा औषधि उद्योग में मौजूद है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विजन तथा कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है।
Rising divorces a sign of justice, not arrogance
SA Aiyar
RSS chief Mohan Bhagwat has made headlines by saying divorce is commoner in educated and affluent families “because with education and affluence comes arrogance, as a result of which families fall apart.” In the ancient days that Bhagwat reveres, India had affluent and educated men. It did not have affluent, educated women. They were denied equal inheritance rights and education, and kept at the complete mercy of male masters. Social customs meant women could not stand independently on their two feet, so divorce was not an option.
Education makes people uppity and demand rights, and this outrages those with power. In the era of US slavery, laws made it a crime to educate slaves, for education might give the blighters notions of freedom or equality. In British India, Macaulay and other grandees in London sought to create a cadre of educated Indians to help run the colony. But that idea was hated by the British stationed in India, who loved illiterate peasants (that posed no threat) but hated educated Indians (who were uppity enough to talk of independence).
Ancient Hinduism had no formal divorce procedures. But women could be thrown out by their husbands even on the most outrageous grounds or false rumours (ask Sita).
Bhagwat should celebrate the fact that such terrible gender inequality is now forbidden by the Indian Constitution. This declares there can be no discrimination on the grounds of religion, caste, race, sex, or place of birth. Sadly, all ancient traditions — including Hinduism, Islam, Christianity and other faiths —practised all these forms of discrimination. The grey eminences that formulated the Constitution were educated, affluent and arrogant enough to ban the traditional discriminations of all religions.
Hindu tradition gave males power over property, marriage, occupation and all family matters. Marriages were financial deals between parents entailing dowry payments. Child marriage was standard. Katherine Mayo’s ‘Mother India’ lists examples of six-year-old girls hospitalised with crushed pelvises after forced sex with older husbands, who nevertheless wanted their wives back to meet their sexual needs.
Sati condemned women to be burned on the funeral pyres of their late husbands. Men were not expected to immolate themselves on their late wives’ pyres.
Fortunately, women are getting educated and affluent, and are no longer helpless pawns. They can think and act for themselves, including shedding undesirable husbands. Rising divorces are a sign that male tyranny is finally getting contested and punished. This is justice, not arrogance.
A Family Health Survey revealed that one-third of women above 15 years had suffered domestic violence, with broken bones, teeth and eye injuries. Yet only 14% of the sufferers sought to stop it. The good news — Bhagwat may disagree — is that women who went to school are more likely to report violence and will hopefully dump their torturers.
Every faith and tradition has a damnable record of oppressing women. Islam requires a raped woman to produce four witnesses, making it almost impossible for her to complain. Instant triple talaq is an outrage. Many Islamic countries force women to stay home and never move out unless accompanied by a male relative. In Iran, women cannot watch a football match because that will allow them to see exposed men’s legs, and that, apparently, will destroy Islamic society.
A Human Rights report in 2010 in Pakistan says almost 800 women were victims of “honour killings”. Tradition empowered village elders to order the rape, murder or barter of women for love affairs involving them or family members. India is not much better — honour killings continue here too.
Christianity discriminated against women too. Through most of history, Christian countries gave males a monopoly of property and other rights. St Thomas Aquinas, a great philosopher, declared that rape was less sinful than masturbation because rape contained the possibility of procreation, a noble Christian cause, while masturbation did not.
Roman Christian Emperor Constantine defined elopement as rape. If the female had consented, she was burned at the stake along with her male friend. If she had not consented, she was still considered an accomplice on the grounds that she could have saved herself by screaming for help.
Another terrible Christian tradition declared old widows to be devil-worshippers and witches, and so burned alive. The accusations were often brought by greedy male relatives wanting to seize the women’s property.
Fortunately, Europeans have now become affluent and educated enough to become what Bhagwat calls “arrogant”. They denounce ancient traditions as terrible crimes.
Bhagwat is educated and reasonably affluent. Let’s hope this makes him arrogant enough to denounce the many Hindu customs that mistreated women shamefully in the name of tradition.
Date:23-02-20
West is selective on refugees, so why scoff at India for CAA?
Swapan Dasgupta
Last week, the United Kingdom — now free from the norms set by the European Union — announced its new immigration policy. Loosely based on the points system that is in vogue in Australia, it is aimed at ensuring that individuals with skills and those who will not burden the welfare system are accorded priority.
One of the features of the new policy is the importance attached to a potential immigrant being familiar with the English language. Inevitably, this insistence on a knowledge of English has drawn criticism from those who feel it is culturally biased. However, it is a policy that has been formulated by a democratically elected government that had a new immigration policy in its election manifesto.
The right of a sovereign nation to determine who to allow to settle and work has never been seriously contested. Last week, for example, Israel facilitated the entry of a packed plane load of Ethiopian Jews as part of its ‘right of return’ policy for all Jews throughout the world. The ‘right of return’ is a foundational doctrine of Israel. UK, Ireland and Germany too have conceded the rights of individuals who can demonstrate national ancestry to settle in these countries. Indeed, after Brexit there has been a rush of people of Irish origin living in the UK to acquire Irish passports.
Conversely, the right to select immigrants has also extended to determining who not to allow into the country. Hungary has consistently defied all EU directives and refused to settle any refugees from Iraq, Syria and North Africa on the grounds that such people wouldn’t fit in. Other East European countries such as Poland, the Czech Republic and Slovakia have also made their displeasure at having to accommodate these refugees quite apparent.
Although in 2015, Germany — out of an exaggerated sense of historical guilt — quite indiscriminately accepted some 8,00,000 alleged victims of war from countries that it doesn’t even share borders with, most countries have insisted on the principle of selectivity. This includes the United States which has an impressive track record of telling other countries how to conduct their affairs of state. In 1990, the US Senate passed an amendment moved by Frank Lautenberg that fast-tracked the immigration of Jews and certain Christian denominations from the erstwhile Soviet Union. Individuals from these communities were not required to individually demonstrate that they were victims of religious persecution. Subsequently, in 2004, this law was extended to include members of the Bahai community in Iran.
What prompted senator Lautenberg to press for special rights for some communities, to the exclusion of others, was the bitter experience of Jews in Germany under Hitler. In the 1930s, this exceptionally targeted community, millions of whom were subsequently to perish in the gas chambers, had to wait in a normal queue to be given the right to emigrate to the US. Their desperation to get away from Nazi-held Europe wasn’t factored in. The story may have well been different if the US had accommodated the special requirements of European Jewry, just as it subsequently did for the persecuted religious communities of the former Soviet Union and Iran.
It is in this context that the pronouncements of the US Commission on International Religious Freedom (USCIRF) on India’s Citizenship Amendment Act appears disingenuous. Given its own precedents, it cannot with a straight face censure India for extending fast-track citizenship to minority communities from three neighbouring countries who have already fled to India. Neither can it realistically contend that religious minorities never suffered to their well-being for professing their faith. The religious persecution of Christians in Pakistan, for example, has attracted enormous attention in the West and many of them charged with blasphemy have been given refuge in Europe, Canada and the US. Instead, it has fallen back on individual pronouncements by political activists to suggest that the CAA could — not that it does — become a template to deprive Muslims of Indian citizenship. Its fears are based on hypothetical developments.
Nevertheless, the USCIRF has encouraged four distinct trends that underpin the anti-CAA protests: the assertion that there was no real religious persecution in the Islamic states, that Hindu refugees from Bangladesh be treated on a par with the illegal Muslim migrants who came in search of better opportunities, that Muslim Rohingyas from Myanmar be allowed to settle and acquire Indian citizenship and, finally, that India should maintain either a soft or an open border with its neighbours. These are highly politically contentious demands that go against the tenets of India’s nationhood and sovereignty.
The next mission
Like Swachh Bharat, Jal Jeevan Mission will benefit the wider economy
Parameswaran Iyer, [The writer is secretary, Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti]
Last month, I had the opportunity to present the key learnings from the Swachh Bharat Mission (SBM) at the ministerial round table discussion on “scaling up sanitation in Africa” at Addis Ababa. While the ministers of sanitation from the African countries of Ethiopia, Nigeria, Kenya and Senegal marvelled at India’s astronomical success in tackling open defecation in just five years, they unanimously agreed that one of the biggest hurdles they faced in replicating the SBM model in their countries was that they were not able to convince their finance ministries to invest heavily in sanitation like India has done since 2014. The unspoken assumption was that they had not received political support from the highest level for scaling up sanitation in their countries.
In India, the prime minister’s leadership in championing a hitherto neglected subject like sanitation has been unquestionably the key ingredient for success of SBM. This then triggered the large investment on sanitation through public financing. We have been very fortunate that since 2014, our finance ministers saw the importance of investing in sanitation and its far reaching heath, economic and environmental benefits. Hence, the central and state governments have invested in excess of one lakh crore on sanitation over the past five years. A majority of these funds have gone towards incentivising the poor and marginalised households to construct and use household toilets, bringing about behaviour change, and building capacities of field functionaries. Over 10 crore toilets have been built in rural India and nearly 55 crore people have stopped defecating in the open, all in just five years. This has contributed in bringing down global open defecation by more than half.
The returns on these investments have been manifold, and their effects on the broader economy, markets and employment have been significant. The UNICEF recently estimated that investments in sanitation in India are yielding a 400 per cent return with each rural household in an open-defecation-free village saving Rs 50,000 on account of avoided medical costs and time savings. The Toilet Board Coalition has estimated that the sanitation infrastructure and services market in India will be worth over $60 billion by 2021, many new jobs, even in the most rural areas of the country, apart from reducing health and environmental costs and generating savings for households. Many people engaged in the business of manufacturing toilet related hardware accessories have reported huge growth in sales during the SBM period. They project a continued uptrend through retrofitting and upgrades. This has been corroborated by another recent study by UNICEF in which they have estimated that SBM has resulted in creating over 75 lakh full time equivalent jobs over the past five years, giving the rural economy a major boost.
It is fairly clear now that investment in sanitation is actually a facilitator for broader economic, health and social gains. This is the chain of arguments that we encouraged the sanitation ministers of Africa assembled at Addis Ababa to use to bring their finance ministries on board.
Back home, our government continues to prioritise the water and sanitation sectors as key pillars of broader rural development. The government is committed to ensuring that this success is sustained. On October 2, 2019, the prime minister, when commemorating the ODF declaration by all states, said that this is but a milestone and not the finish line, and that we must all ensure that people continue to use toilets and that no one is left behind. This has been backed up by the finance minister in the budget for 2020-21, wherein she announced about Rs 10,000 crore for rural sanitation to focus on ODF sustainability, bio-degradable waste management, greywater management, fsludge management and, critically, plastic waste management for all villages by 2024.
The next critical basic service, and arguably the most aspirational of them all, that this government is committed to delivering, is piped water supply. On Independence day this year, the prime minister announced the Jal Jeevan Mission (JJM) from the ramparts of the Red Fort with the goal of ensuring piped water supply for all households of India by 2024 and with a commitment of Rs 3.6 lakh crore of central and state funds for the scheme. In the Union budget for 2020-2021, the government has already allocated Rs 11,500 crore for JJM, with an additional Rs 12,000 crore being made available through extra budgetary resources.
In addition, a huge impetus to the rural water supply and sanitation sector is the earmarking of 50 per cent of the Rs 60,750 crore grant for rural local bodies provided under the Fifteenth Finance Commission for drinking water and sanitation. This will ensure that the gram panchayats and local communities have more skin in the game, and are responsible for the upkeep of their water and sanitation infrastructure, providing a boost to the sustainability of service delivery to people. This approach will ensure that just like sanitation, provision of water supply and its upkeep will also become everyone’s business.
मुनाफे का गणित और खतरे की घंटी
आलोक जोशी
इंसान फोन लेता है बात करने के लिए। जिस कंपनी का यह विज्ञापन था, कुछ समय बाद उसने ही फिर बताया- इंसान बात करता है तरक्की के लिए। और एक अन्य साहब थे, जो सबको बताते थे कि कहां-कहां और कैसे-कैसे तरक्की हो सकती है, एक छोटे से मोबाइल के रास्ते। लोगों ने बात पकड़ ली। न सिर्फ तरक्की, बल्कि मनोरंजन, राजनीति और अपने सारे हिसाब सलटाने का हथियार भी बना डाला मोबाइल को। लेकिन इसमें कुछ झोल हो गया। और उसी का नतीजा है कि देश भर के लोगों की तरक्की की जिम्मेदारी उठाने वाला टेलीकॉम सेक्टर आज एक तरह से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। पिछले 20 साल में देश की 20 से ऊपर टेलीकॉम कंपनियां बंद हो चुकी हैं।
खास बात यह है कि इस दौरान कारोबार लगातार बढ़ता रहा। इस वक्त आइडिया-वोडाफोन के पास करीब 30 करोड़ और एयरटेल के पास लगभग 28 करोड़ कनेक्शन हैं। दोनों मिलकर भारत के टेलीकॉम कारोबार में 60 फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदार हैं। लेकिन ये दोनों घाटे में हैं। पिछली तिमाही में भारतीय एयरटेल को लगभग एक हजार करोड़ रुपये और आइडिया-वोडाफोन को करीब साढे़ छह हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। ये कारोबारी घाटा है। इसकी एक बड़ी वजह इस धंधे में मौजूद तीसरा बड़ा खिलाड़ी है- रिलायंस जियो। पिछले डेढ़-दो साल से इस कंपनी ने जियो के सिम, जियो के कनेक्शन और डाटा या कॉल प्लान दूसरों से बहुत सस्ते में बांट-बांटकर खूब सारे ग्राहक जोडे़ हैं। और उससे मुकाबले के चक्कर में सामने खड़ी ये दोनों कंपनियां भी रेट कम करते-करते इस हाल में पहुंच गईं। रिलायंस जियो अब देश की इकलौती टेलीकॉम कंपनी है, जो फायदे में चल रही है।
कहा जाता है कि जब मुसीबत आती है, तो अकेली नहीं आती। थोड़ा पीछे चलें, तो किस्सा वहां से शुरू होता है, जिसे पिछली सरकार का सबसे बड़ा घोटाला बताया जाता है, यानी 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला। भारत सरकार के सबसे बडे़ ऑडिटर यानी सीएजी ने यह भंडाफोड़ किया था कि तब के टेलीकॉम मंत्री ए राजा ने मनमाने तरीके से मोबाइल टेलीफोनी के लिए स्पेक्ट्रम का अधिकार बांटा और इससे सरकारी खजाने को एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह बड़ी रकम थी, और विनोद राय जैसे काबिल अधिकारी की राय थी, तो पूरे देश ने इसे गंभीरता से लिया। जो बवाल मचा, जो राजनीति हुई और उसका जो नतीजा हुआ, वह आज सबके सामने है।
लेकिन यह बात अब लगभग पूरी तरह खुल गई है कि जितने बड़े नुकसान का अंदाजा लगाया गया था, वह सही नहीं था। ज्यादातर विद्वान इस बात पर एकमत हैं। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है। जिन कंपनियों के लाइसेंस पर सवाल थे, उनमें से ज्यादातर बंद हैं, कुछ के मालिक तो जेल जा चुके हैं और उनके दूसरे धंधे भी बरबाद हो चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई है कि दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के मन में आशंका पैदा हो गई कि भारत में पैसा लगाना बडे़ जोखिम का काम है। वोडाफोन ने तो फिर भी हिम्मत दिखाई, और इसी तरह एयरटेल के विदेशी पार्टनर सिंगापुर टेलीकॉम, यानी सिंगटेल ने भी भारत पर भरोसा नहीं खोया। शायद इसलिए कि इन कंपनियों का यहां काफी कुछ दांव पर था। इसी भरोसे के कारण पिछले साल आइडिया-वोडाफोन के राइट्स इशू में करीब 25 हजार करोड़ रुपये उसके प्रोमोटरों ने ही लगाए। उन्हें अंदाजा था कि मार्च 21 तक कंपनी को करीब तीस हजार करोड़ रुपये और खर्च करने पड़ सकते हैं। मगर यह हिसाब बिगड़ गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। कंपनियों को कुल मिलाकर करीब 1.40 लाख करोड़ रुपये चुकाने का हुक्म मिल गया।
दरअसल, संचार विभाग और मोबाइल या टेलीकॉम कंपनियों में समझौता है कि कंपनियां अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को या संचार विभाग को देती रहेंगी। इससे उन पर एक साथ भुगतान का बोझ नहीं पड़ता और यदि कारोबार काफी तेज हो जाए, तो सरकार को भी नुकसान न होता। लेकिन झगड़ा हो गया इस बात पर कि कमाई का हिसाब कैसे लगाया जाए? सरकार ने हिसाब जोड़ा कि टेलीकॉम लाइसेंस लेने वाली कोई भी कंपनी जितनी भी कमाई करेगी, उस पूरी कमाई में से हिस्सा देना होगा, जबकि कंपनियों का तर्क है कि सिर्फ टेलीकॉम कारोबार से होने वाली कमाई का ही हिस्सा बांटा जाए। इस गणित का ही नतीजा है कि ऑयल इंडिया, पावर ग्रिड और गैस अथॉरिटी जैसी सरकारी कंपनियों पर भी कुल मिलाकर करीब तीन लाख करोड़ रुपये की देनदारी निकल आई है, जबकि वे टेलीकॉम से कमाई या तो नहीं करती हैं या फिर न के बराबर। उनसे यह हिस्सा सिर्फ इसलिए मांगा जा रहा है, क्योंकि उनके पास टेलीकॉम लाइसेंस है, जो उन्होंने इस उम्मीद में लिया था कि शायद भविष्य में कभी वे ऐसा कोई इंतजाम खड़ा करें, जिससे कमाई हो सकती हो। इन कंपनियों का मामला तो टीडीसैट में है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे रखी है। सवाल उठ रहा है कि फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी कमाई में से भी संचार विभाग क्या यह हिस्सा मांग सकता है?
एयरटेल ने तो पैसा भरना शुरू भी कर दिया है। लेकिन खासकर आइडिया-वोडाफोन के लिए यह बड़ी मुसीबत है। उसे करीब पचपन हजार करोड़ रुपये सरकार को चुकाने हैं। खबर है कि यह रकम और बढ़ सकती है, क्योंकि सरकारी अफसरों ने अभी साल 2017 के बाद की देनदारी का हिसाब तो जोड़ा ही नहीं है। अगर कंपनी यह रकम नहीं भर पाई, तो वह बंद हो जाएगी, लेकिन सरकार की भी इतनी बड़ी रकम डूब जाएगी। इसी कंपनी ने अनेक बैंकों से, जिनमें स्टेट बैंक भी है, करीब पचास हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले रखा है, कंपनी दिवालिया हो गई, तो उसकी वसूली भी मुश्किल।
यहां यह बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि कमाई में हिस्से का फॉर्मूला 1999 में बना था, जबकि स्पेक्ट्रम की नीलामी 2010 के बाद से हो रही है। तो यह गणित ही सवालों के घेरे में है। अभी सरकार बीएसएनएल को 70 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दे चुकी है। फिर उसे आइडिया-वोडाफोन को राहत देने का रास्ता क्यों नहीं निकालना चाहिए? खासकर तब,जब इस कंपनी के बंद होने में सरकार और ग्राहकों का भी बड़ा नुकसान है।