
22-09-2017 (Important News Clippings)
To Download Click Here.

निहायत ही आवश्यक है प्रशासन में सुधार
डॉ० विजय अग्रवाल
इनके अतिरिक्त भी वर्तमान सरकार ने नौकरशाही को सक्षम और ईमानदार बनाने के लिहाज से कुछ अन्य व्यावहारिक कदम उठाये हैं। इनमें अपनी सम्पत्ति का खुलासा करना, विदेशों की यात्रा पर नियंत्रण, प्रशिक्षणों की अनिवार्यता के साथ-साथ उन पर लगातार निगरानी रखना भी शामिल है। यही कारण है कि राज्यों के अब तक के कई योग्य आईएएस अफसरों को जब केन्द्र में अतिरिक्त सचिव एवं सचिव पद के इम्पैन्लमेंट के लिए जाँचा-परखा गया, तो वे इसके लिए अयोग्य पाये गये। कुल मिलाकर यह कि सरकार के जिन उच्च पदों पर ये अधिकारी अपना कैरियर सिद्ध अधिकार मानकर निश्चिन्तता की बाँसुरी बजाया करते थे, अब वे दिन लदते हुए नजर आ रहे हैं।इतना ही नहीं, बल्कि केन्द्र की वर्तमान सरकार अब सामान्यज्ञ की जगह विशेषज्ञों पर अधिक भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति को लेकर आई.ए.एस. अफसरों में काफी रोष है, और वे इस नीति का हरसंभव विरोध करने में भी लगे हुए हैं। जाहिर है कि ऐसे कामों को खुले रूप में अंजाम नहीं दिया जाता है।निजी क्षेत्र के लोगों को सरकार में लाने की बात तो खैर थोड़ी-बहुत दुखदायी हो भी सकती है। लेकिन आई.ए.एस. लॉबी को तो अपने समान स्तर पर वे अधिकारी भी बर्दाश्त नहीं होते, जिनका चयन उन्हीं वाली परीक्षा के आधार पर हुआ है। बस, परीक्षा में उनके नम्बर कम आ गए थे, और वे भी बहुत थोड़े से ही कम। यह थोड़ी दिलासा देने वाली बात है कि वर्तमान में कुल 93 सचिव के पदों पर 20 सचिव गैर आई.ए.एस. हैं। विभिन्न सरकारी सेवाओं के बीच का संतुलन मनोवैज्ञानिक एवं दक्षता की दृष्टि से प्रशासनिक सुधार का एक आवश्यक पक्ष है।
आजादी के बाद के सत्तर साल के भारत के विकास के संदर्भ में अक्सर एक बात कही जाती है कि असफलताओं का मूल विधायन में उतना नहीं है, जितना उसके लागू किये जाने में। अब तक संविधान में किये गये लगभग सवा सौ संशोधनों से अधिक नीतिगत लचीलेपन का प्रमाण अन्य क्या हो सकता है। लेकिन बात जब उंगली उठाने की होती है, तो आम जनता तक का इशारा राजनेताओं की ओर होता है। नौकरशाहों को वह दोषी ठहराती तो है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में। बल्कि जो लोग ‘देने के मामले’ में सक्षम होते हैं, वे तो ऐसा भी नहीं करते, क्योंकि इस तरह के नौकरशाह इनके लिए बहुत एवं अतिरिक्त रूप से सुविधाजनक एवं लाभकारी होते हैं।
राजनीतिक नेतृत्व ने जितना ध्यान नई-नई नीतियों को बनाने पर दिया है, उसका चैथाई हिस्सा भी उसे लागू करने वाले प्रशासन तंत्र पर नहीं दिया गया। सत्तर सालों के दौरान केवल दो प्रशासनिक सुधार आयोग बनाये गये। उनकी भी सिफारिशों को विशेष तवज्जो नहीं दी गई। फलस्वरूप थेड़े-बहुत कास्मेटिक परिवर्तनों के साथ प्रशासन का मूल ढाँचा और चरित्र उपनिवेशवादी काल का ही बना रहा। इसके कारण राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक चरित्र एवं समाज की आवश्यकताओं के बीच न केवल अंतराल ही आता चला गया, बल्कि टकराव की स्थितियां भी निर्मित होने लगी। इस टकराव का जो व्यावहारिक किन्तु अवैधानिक समाधान निकाला गया, वह ‘‘क्रोनी कैप्टीलिज्म’’ के रूप में सामने आया। यह ‘‘अंतराल एवं टकराव’’ से भी खराब स्थिति थी।इस एक अन्य खराब स्थिति पर भी गौर किये जाने की जरूरत है कि प्रशासन तंत्र में सुधार लाने के जो भी थोड़े-बहुत प्रयास दिखाई दे रहे हैं, वे केन्द्र सरकार के स्तर पर ही हैं। राज्यों में इस बारे में न तो कोई हलचल है, और न ही कोई बेचैनी। जबकि जनता का जितना सीधा संबंध राज्यों के प्रशासन से होता है, उसका शायद एक प्रतिशत संबंध ही केन्द्र से होता हो। इसलिए आम लोग केन्द्रीय स्तर पर होने वाले सुधारों के अनुभव से अब तक पूरी तरह वंचित ही हैं। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक अभी भी उनके ‘माई-बाप’ और ‘सरकार’ ही बने हुए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस तरह के किसी भी सुधार एवं अनुशासन से पूरी तरह अप्रभावित हैं, जिनकी संख्या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की संख्या से कई गुना ज्यादा है। और ये ही वे हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर ‘राज’ करते हैं।यहाँ मैंने जानबूझकर ‘माई-बाप’ और ‘राज’ शब्द का प्रयोग किया है।
दरअसल इन शब्दों का संबंध प्रशासकों की उस मानसिकता से है,जो उन्हें सीधे-सीधे ब्रिटिश सत्ता तथा सामंतवादी समाज से प्राप्त हुई है। सैद्धांतिक रूप से ये भले ही ‘सिविल सर्वेन्ट’ कहलाते हों, लकिन मूलतः इनका व्यवहार और आचरण ‘सिविल मास्टर’ से कम नहीं होता। चूंकि हमारी जनतांत्रिक राजनीति स्वयं भी इसी मानसिकता का सुखभोग करती है, इसलिए इसमें परिवर्तन की संभावनायें भी दिखाई नहीं देतीं। लाल बत्तियों के अंत को इस दिशा में उठाये गय ठोस कदम का आरम्भ माना जा सकता है। ‘न्यूनतम सरकार’ की अवधारणा के मूर्तिकरण से ऐसी मानसिकता पर प्रतिबंध लग सकता है, जिसके लिए अधिकारों के विकेन्द्रीयकरण की आवश्यकता होगी। साथ ही अधिकारों के संतुलन की भी।इस बारे में हमें इस एक अत्यंत कटु एवं अप्रत्यक्ष सत्य को भी स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक सुधार की नाल कहीं न कहीं राजनीतिक सुधारों से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। सच तो यह है कि एक साफ-सुथरा राजनीतिक नेतृत्व बिना कुछ किये और कहे अपने आप ही प्रशासन में काफी कुछ सुधार ला देता है। शायद यही वह सबसे बड़ा कारण है, जो अब तक के प्रशासनिक सुधारों के रास्ते का अरावली बना हुआ है।
 Date:22-09-17
Date:22-09-17
Embrace reforms
More than a stimulus, reversing economic slowdown needs factor market unshackling
TOI Editorials
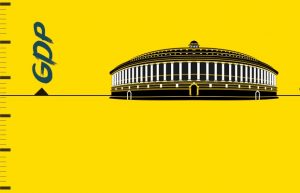
For sure, there should be a package of short-term measures to address specific problems which hamper exporters and other economic actors. But what India really needs is a sustained effort to transform its economic architecture. The 1991 reforms, which can be characterised as measures which unshackled India’s product markets, have played their part and their momentum is exhausted. The next stage of reforms must transform India’s markets for factors of production such as land, labour and capital. In this context, the Modi government’s introduction of a bankruptcy law can serve as a template as it can significantly enhance the efficiency with which capital gets allocated.
An economic transformation to create a ‘new India’ is not going to come about with the prevailing legal framework which governs transactions in land and hiring of industrial labour. As highlighted by Rahul Gandhi, inadequacy of decent jobs continues to remain a problem as it did in UPA’s second term; it may, in fact, have gotten worse. Disinvestment hasn’t taken off, while areas such as education and agriculture have barely been touched by the 1991 reforms. Ease of doing business must improve radically. GST structures are extremely complicated and needs to be simplified; diesel and petrol should be brought within GST. Given BJP’s political dominance, it is imperative that Prime Minister Narendra Modi uses his considerable political capital to pilot economic transformation. Else ‘new India’ and ‘acche din’ will remain hollow promises.
देश विश्व अर्थव्यवस्था का इंजन बनने को तैयार
उचित नीतियां बनाई गईं तो हमारा किफायती इनोवेशन और ठोस बुनियाद तेज चाल को छलांग में बदल देंगे।

 Date:22-09-17
Date:22-09-17
छोटी-मझोली कंपनियों के लिए कारोबारी सुगमता से बनेगी बात
कनिका दत्ता
कारोबारी सुगमता के मामले में भारत की प्राथमिकताएं लगातार गलत दिशा में जाती दिख रही हैं। कारोबारी सुगमता संबंधी वैश्विक रैंकिंग पर नजर डालते ही हम इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपनी निवेश पूंजी को भारत से बाहर नहीं ले जाने तक सीमित मान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके उच्च-शिक्षित आर्थिक विशेषज्ञ अगर बड़ी कंपनियों के बजाय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर ध्यान केंद्रित करें तो बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं। एमएसएमई क्षेत्र के लिए कारोबार करना हमेशा से कठिन रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अकेले एक तिहाई का योगदान करने वाले इस क्षेत्र के लिए कामकाज कर पाना आम तौर पर मुश्किल ही बना हुआ है। रोजगार प्रदान करने के मामले में भी यह भारतीय अर्थव्यवस्था का चमकदार क्षेत्र है। वहीं बड़ी कंपनियां अपनी मजबूत संस्थागत क्षमताओं और रसूख के बावजूद ऐसा नहीं कर पाती हैं। शायद इसी वजह से भारत हर साल इस रैंकिंग में समतुल्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में पिछड़ता जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र की स्थिति एक भीमकाय पशु जैसी है। यहां पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए कई तरह के कटऑफ रखे गए हैं जिनमें 25 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपये तक की निवेश सीमा है। एमएसएमई क्षेत्र ऐसे परिवेश में काम करता है जो काफी हद तक संगठित अर्थव्यवस्था से बाहर है और उसके बारे में सटीक आंकड़े जुटा पाना भी मुश्किल है। स्थानीय भ्रष्टाचार का सबसे अधिक सामना इसी क्षेत्र को करना पड़ता है। श्रम एवं कारखाना निरीक्षक भारतीय संस्कृति में खलनायक का ओहदा हासिल कर चुके हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में सक्रिय उद्यमियों को अपना कारोबारी वजूद बचाए रखने के लिए विकृत व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी बूचडख़ानों का तीव्र प्रसार होना कारोबारी सेहत के लिए नुकसानदेह परंपराओं को बढ़ावा देने वाली नियामकीय प्रणाली का एक सटीक उदाहरण है।छोटी एवं मझोली इकाइयां चलाने वाले उद्यमियों ने 1980 के दशक से ही लगातार कहा है कि उन्हें बैंकों से आसान शर्तों पर कर्ज के बजाय बेहतर कामकाजी माहौल चाहिए। उदारीकरण के पहले इन उद्यमियों की चिंता बिजली और फोन कनेक्शन हासिल करने जैसी बुनियादी सुविधाएं होती थीं। फिर 1990 के दशक से उनका सरोकार कारगर कामकाजी ढांचा खड़ा करने का रहा है लेकिन नियामकीय व्यवधानों की अधिकता, बाजार पहुंच बढ़ाने और कर अनुपालन संबंधी नियम भी चिंता का विषय बन गए हैं।
पिछले एक साल में इस क्षेत्र के लिए हालात काफी प्रतिकूल हुए हैं। एमएसएमई क्षेत्र की गतिविधियों को राष्ट्रीय आर्थिक आंकड़ों में इस तरह से पेश किया जाता है कि उनके संकट की गंभीरता का अहसास ही नहीं हो पाता है। हम आर्थिक विकास की धीमी पड़ती रफ्तार और बढ़ती बेरोजगारी के आंकड़ों से ही यह अंदाजा लगा पाते हैं कि इस क्षेत्र की हालत कितनी खराब हो चुकी है। यह अलग बात है कि कुछ अर्थशास्त्री इन आंकड़ों से असली तस्वीर बयां हो पाने को लेकर आश्वस्त नहीं हैं।नोटबंदी ने एमएसएमई क्षेत्र पर गहरी चोट की। खासकर रोजमर्रा पर काम करने वाली बेहद छोटी इकाइयों के लिए तो नोटबंदी घातक साबित हुई। जो इकाइयां इस वार को झेल पाने की स्थिति में थीं, उन्हें पुराने नोटों को बदलवाने के लिए 30 फीसदी तक कमीशन देना पड़ा। गत 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान होने के साथ ही पुराने नोट ठिकाने लगाने वाला एक पूरा गिरोह ही अचानक पैदा हो गया था। स्थानीय बाजारों में नकदी नहीं होने से छोटी इकाइयों को अपना कामकाज समेटना पड़ा था। इसका असर यह हुआ कि बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक अपने गांवों की ओर लौटने को मजबूर हुए।
कुछ महीने बाद ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से एमएसएमई इकाइयों पर दोहरी मार पड़ गई। किसी पूर्व-परीक्षण के बगैर जीएसटी को लागू किए जाने के एक ही महीने के भीतर इसकी खामियां नजर आने लगीं। बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी की अगुआई में एक समिति बनाई गई जो जीएसटी में आने वाली अड़चनों को दूर करने के उपाय सुझाएगी। जीएसटी से संबंधित तकनीकी उलझन और दोषपूर्ण ढांचे ने पहले से ही परेशान उद्यमियों और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए दु:स्वप्न की स्थिति पैदा कर दी। इससे एमएसएमई क्षेत्र की मुश्किलें और भी बढ़ गई क्योंकि उनमें से काफी इकाइयां जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।
यह काफी दुविधापूर्ण स्थिति है। एमएसएमई इकाइयों को कर प्रणाली में शामिल करने से लागत और जटिलताएं दोनों ही बढ़ जाएंगी। वहीं इन्हें दायरे से बाहर रखने का मतलब है कि इस क्षेत्र की छोटी इकाइयों को खरीदार ही नहीं मिल पाएंगे। ब्रांडेड उत्पादों पर कर लगाने और गैर-ब्रांडेड उत्पादों को दायरे से बाहर रखने जैसी सीमित सोच छोटी इकाइयों को अपना ब्रांड बनाने से परहेज करने के लिए मजबूर करेगी। अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर निरमा जैसे स्थानीय ब्रांड का उभर पाना खासा मुश्किल होगा। उद्यमी खुद को जीएसटी के मुताबिक ढालने में ही लगे हुए हैं। जीएसटी पर बिज़नेस स्टैंडर्ड की तरफ से आयोजित राउंड टेबल में भी उद्यमियों ने ऐसी ही चिंताओं और नाराजगी का इजहार किया था। सत्ता प्रतिष्ठान कारोबारियों और उद्यमियों की चिंताओं के प्रति अनिच्छुक नजर आया। अगर सरकार को अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करनी है तो उसे एमएसएमई क्षेत्र पर पड़ रहा बोझ कम करने पर ध्यान देना चाहिए। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल दलों की ही अधिकांश राज्यों में सरकारें होने से ऐसा कर पाना मुश्किल भी नहीं होगा।सरकार ने कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत को 130वें स्थान से 90वें स्थान तक लाने का लक्ष्य रखा है। इस बड़ी सोच को पूरा करने के लिए उसे छोटे कारोबारियों से इतर कहीं और देखने की जरूरत नहीं है।
Date:22-09-17
सुदृढ़ीकरण पर ध्यान
संपादकीय
अब यह स्पष्ट हो चला है कि देश की अर्थव्यवस्था की वृद्घि दर में कमी आ रही है। वर्ष 2016 के आरंभ से लगातार छह तिमाहियों में गिरावट आई है। ताजातरीन आंकड़े 5.7 फीसदी की वृद्घि दर के हैं जो बीते कई सालों में सबसे कमजोर है। यह अप्रैल-जून तिमाही के सालाना आधार पर प्रस्तुत आंकड़े हैं। ऐसे में यह अच्छी बात है कि आखिरकार सरकार अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के तरीके तलाशती दिख रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अन्य मंत्रालयों के सहयोगियों से मुलाकात के बाद कहा है कि सरकार इस मंदी के खात्मे के लिए जरूरी अतिरिक्त कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद ये कदम सामने लाए जाएंगे। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि ये उपाय केवल अतिरिक्त व्यय बनकर नहीं रह जाएंगे बल्कि नीतिगत खामियों को दूर करेंगे और अतीत की कमियों की भरपाई करेंगे।इससे पहले भी मौद्रिक और राजकोषीय नीति के स्तर पर कदमों की मांग उठी थी। ब्याज दरों का निर्धारण आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति करती है और वह मूल्य आधारित संकेतों पर निर्भर रहती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने यह स्पष्टï कर दिया है कि जहां तक उच्च वृद्घि दर कायम करने की बात है तो गेंद सरकार के पाले में है। परंतु राजकोषीय नीति की शिथिलता खतरनाक साबित होगी। सरकार को राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ पर विश्वसनीयता कायम करने में मेहनत करनी पड़ी है। नीति आयोग की तीन वर्षीय कार्य योजना और मध्यम अवधि के राजकोषीय खाके समेत जरूरी दस्तावेजों में लगातार इस बात पर जोर दिया गया है कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखा जाए। बहरहाल वर्ष 2013 जैसी स्थिति बनती नहीं दिखती जब देश की अर्थव्यवस्था भुगतान संतुलन के घाटे के कगार पर पहुंच गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। परंतु वृहद आर्थिक स्थिरता कमजोर है और यह काफी हद तक कमजोर तेल कीमतों की आपूर्ति और विदेशी मुद्रा की निरंतर आवक पर निर्भर है।अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया है कि वह अपने बॉन्ड खरीद कार्यक्रम को बंद करेगा। ऐसे में भारत जैसे देश के लिए राजकोषीय संयम से दूरी बनाना गैरजवाबदेही का परिचायक होगा। चाहे जो भी हो राजकोष दबाव में है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने इसे प्रभावित किया है। नई कर व्यवस्था ने भविष्य के राजस्व को लेकर अनिश्चितता पैदा की है। यह अनिश्चितता केंद्र और राज्य दोनों के लिए है। इन अनिश्चित हालात में कोई नई व्यय योजना पेश करना उचित नहीं होगा।
इस समय पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि कैसे सरकार दिए गए साधनों में काम करती है। केंद्र सरकार को इस गलत धारणा के साथ सुधार का वादा नहीं करना चाहिए कि वह खर्च करके वृद्घि की दशा बदल सकती है। वह अतीत में पहले ही ऐसे विचार के मामले में कमजोर साबित हो चुकी है। तेल के मोर्चे पर मिलने वाला लाभ समाप्त होने पर हालात का मुश्किल होना तय है। ढांचागत सुधारों की दिशा में काम करना ही एकमात्र विकल्प है। यह उम्मीद भी की जानी चाहिए कि जब सरकार के भीतर सहमति बन जाती है तो श्रम, भूमि और कृषि बाजार को लेकर गहरे सुधारों की ओर काम करना होगा, बजाय कि व्यय में इजाफा करने के। राजकोषीय समावेशन मौजूदा सरकार की अहम उपलब्धियों में से एक है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने 3.2 फीसदी के राजकोषीय घाटे का अनुमान जताया है। अगले वर्ष इसे 3 फीसदी पर लाने की प्रतिबद्घता है। राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन की विशेषज्ञ समिति ने भी इसे वर्ष 2023 तक कम करके 2.5 फीसदी पर लाने की अनुशंसा की है। ऐसे में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ से हटने की मांग को नजर अंदाज करना होगा।
 Date:21-09-17
Date:21-09-17
The Business Of Learning
Affordable education has to be a human right, not a thing to extract profit from.
Parnal Chirmuley,The writer is associate professor, Centre of German Studies, JNU
Advocates of neoliberal economics believe that education needs to primarily be a handmaiden of economic power on the global stage, urging therefore that those branches of education that prove themselves to be economically viable need to be given precedence above all others. In this framework, stocktaking of available strengths becomes essential. One such strength, according to Basu, is the fact that while being colonised may have been terrible for us, we were still mercifully left with the useful old English language. This, and the fact that Jawaharlal Nehru set up IITs, IIMs, and “some fine universities” has led to 1.4 per cent of students participating in Study Abroad programmes out of US universities to choose India as their destination. Fewer than 5,000 students choosing India as a study abroad destination is for Basu good enough reason to “create room for private universities and institutes to flourish” so that “India can become a destination for students from around the world”.
First, in Basu’s own terms, this cannot be sound economics, unless of course endeavours such as these can be funded by private parties, extracting huge profits from those who wish to enrol. Second, our universities have, for decades, welcomed students from all over, but particularly from the global South. These students chose India precisely because solid education was also affordable and accessible because it was supported by the state. This is not the kind of “hub” that Basu argues for. Also, we need no reminding that only a very small section of Indian society has English, it is a marker of both class and caste. Speaking of it in terms of a “strength” is disingenuous.
Basu does indeed go on to say that private firms will invest and that they should be given flexibility on tuition fees and salaries offered to academics to attract the “the best professors”. He tells us that many universities in the US charge upwards of $60,000 as tuition fees, so private universities in India could easily go as low as $20,000 (Rs 12,81,000) “and still make a profit”. Really, who is this education for? For students in the English-speaking global north who don’t make it to universities there, but would still like an education?A big advantage in the education scenario being annexed by private firms is the government needs to do no more than create an enabling environment, so that the return on this “investment will be enormous”, Basu says. It is not clear how these returns on investment made by private firms in commercially viable areas in education will accrue to the state.
In recent years, not only have successive governments in India slashed funding for higher education even as numbers of those who aspire for and enrol has grown exponentially. They have relentlessly pushed the idea of education for profit, paving the way for the retreat of state responsibility at a historical moment when the question of access to education needs far greater attention. In view of students across the country calling for solid and affordable education, institutions of higher learning, some of which rank at the top in the country’s own ranking systems, are being dismantled, bit by bit, both internally and through whipping up of public sentiment against particular universities as being contrary to national interest. These are the very universities that have consistently produced impeccable scholarship that has upheld the principles of equality in society as an objective for the state to uphold. This is not a paradox. The destruction of existing state-funded institutions while publicly arguing for foreign universities is part of the same project that sees education not as a basic human need and right, but as yet another thing to extract profit from, which then circulates only in the hands of a few.
When students across the world are fighting for affordable education, recommending that profit motives eviscerate the noble ideal of education for all is a sign of cultural and political blindness. We need to give hope in education a chance if we want to live in a more equal society where citizens’ human rights are guaranteed.
Date:21-09-17
Behind the 100% swayamsevak
Deen Dayal Upadhyaya’s ideology and political action transcended party lines. He is more relevant today than in his own time
His impact on contemporary political actors can be gauged by his acceptance as an original thinker who transcended party affiliation: Veteran Congressman and a former chief minister of Uttar Pradesh, Sampoornanand, wrote the preface of Upadhyaya’s Political Dairy, which contains social, cultural and political insights. He described Upadhyaya as “one of the most notable political leaders of our time, a man devoted to the good of his country, a person of unimpeachable character, a leader whose weighty words swayed thousands of educated men” and considered Political Dairy essential reading for future political workers.
Is it not a tragedy that the spirit of political socialisation and mutual admiration, which was visible in the 1950s and ’60s, has increasingly eroded? The Nehruvian-left intellectual stream, deluded by its hegemonic status, denied space to diverse thoughts and icons. Our historiography attributed divinity to certain figures and disproportionately glorified their role. Any new inclusion in this pantheon is considered a diminution of Gandhi and Nehru. Research has led to the emergence of many grass-roots women warriors and martyrs from the freedom movement. One of them is Uda Devi. Would the celebration of a Dalit woman patriot be considered a deliberate reduction of Rani Laxmi Bai’s status and role?
Greatness in public life is not measured merely by political success but also by contributions to the advancement of human values, which make democracy virtuous. Indian politics witnessed two contradictory events in the early 1950s. The Congress Working Committee delegated the final say on the selection of more than 4,000 candidates for elections to the Lok Sabha and state assemblies to Jawaharlal Nehru in 1952. That a party with scores of visionaries and leaders felt crippled to contest Nehru’s hegemony shows that its culture of political grooming was weak.
While the Congress inaugurated a personality cult, Upadhyaya demolished this trait before it could take root in the BJS and eventually expelled the party president, Mauli Chandra Sharma, and another veteran leader, Vasant Rao Oak. This tradition can be seen in the symbiotic autonomy of the BJP’s parliamentary party and party organisation. In a democracy, an experiment within a party becomes part of the larger political culture. The Congress and BJP represent two distinct political cultures. While the Congress vice president, Rahul Gandhi, justifies dynastic politics, Modi’s obvious displeasure at the micro-dynasties which infected his party was witnessed during the last election.Upadhyaya’s idealism is more relevant in contemporary India than in his time. In 1963, by-elections were held in four Lok Sabha seats and became a war of prestige between the Congress and the Opposition. Opposition stalwarts, socialists Ram Manohar Lohia (Farrukaabad) and J.B. Kripalani (Amroha), Swatantra Party’s Minoo Masani (Surat) and Upadhyaya (Jaunpur) were in the fray.
Upadhyaya’s victory was considered a forgone conclusion for two reasons: The vacancy occurred due to the death of the sitting BJS MP and caste equations in the constituency were assumed to be in his favour. For Upadhyaya politics was a mission, not a profession. He spoke against caste polarisation and identity-based voting, which led the conservatives to ensure his defeat. However, for him, it was a “victory of the BJS”. He advised parties, “not to sacrifice principles for quick gains” and people to do their duty while exercising their franchise “in a judicious and intelligent manner” to correct the distorted perspective of political parties.
Upadhyaya wanted to decolonise Indian political thought which was largely, as he said, “a Western political picture in the Indian background”. He strongly argued against the left-right division as being detrimental to the growth of a constructive, transformative pro-people ideology. He argued, “this categorisation does not give a correct idea of the politics of India because many programmes of these parties defy any classification on this orthodox basis”.After decades, this view has emerging from many corners of the world. The “creative destruction” he employed for the “third way” led to a greater cohesion between opposing ideas and politics in the 1960s. The BJS, Swatantra Party, socialist parties and the CPI didn’t just form coalitions, the ideological discourse too took a more interactive shape. However, this socialisation was dealt a death blow by the excessive foreign influence on both academia and politics.
Upadhyaya believed that a reactionary politics does not leave the ground for reconstruction and fails to succeed in generating an alternative. He exemplified these beliefs in his political actions. When anti RSS-BJS propaganda by the Indian left was at the centre of the discourse, many wanted to turn the BJS an ideological hub for right-wing politics. Their efforts, however, were in vain. Upadhyaya knew the communists lacked the spirit to Indianise themselves and predicted their decline. He made egalitarianism the first principle of the party, which led to the expulsion of five out of eight BJS MLAs in the Rajasthan assembly opposed to the abolition of zamindari.The Swatantra Party garnered a significant voteshare in the 1962. Following the result, there was a strong move to merge the BJS, the Swatantra Party and Swami Karpatri’s Ram Rajya Parishad (RRP). Upadhyaya raised fundamental questions regarding such a merger: He described the Swatantra Party as a “Dalal Street party” and said that though it was opposed to socialism “it, however, does not know if there can be any better alternative to socialism except the discredited capitalism”. Similarly, the many affinities with their social philosophy did not stop him from writing about the RRP as “a party run not from the cottage of Swami Karpatri ji but from the palace of zamindars and capitalists”, in Panchajanya.
Politics must be controlled by the masses, not the wealthy. Neoliberalism has challenged democracies to ensure they do not become beholden to corporate interests. Upadhyaya cautioned that “if steps are not taken to mend them, powerful lobbies will emerge in the country’s legislatures and political decisions will hardly be taken in an objective manner taking into consideration only the welfare of the people and furtherance of national interests.”Upadhyaya’s “third way” is reflected in his philosophy of integral humanism in which he provided a holistic idea of human welfare. Materialism, spiritualism and cautious desire each have a role in achieving happiness: An economic index cannot be the sole measure of satisfaction or happiness. He pleaded for diversities in economic and social philosophies against a single meta-narrative ruling the world or a nation.Most people have remained ignorant of Upadhyaya’s ideas for decades and now, PM Modi’s emphasis on his thoughts is contested polemically which is pushing India’s public discourse back to a battle between hegemony and counter-hegemony of political ideas. Sampoornanand, while writing the preface for Political Diary, said that the book might be “surprising to some people”.Therefore, it is no surprise that uninformed intellectuals groomed in a culture of political binaries see Upadhyaya merely as a party icon. Sampoornanand’s words are a beacon for contemporary India: He said in the preface to Political Dairy that we must practice “a simple expression of the great virtue of tolerance… if democracy is to take root in our country”.
A big broom — On crackdown on shell companies
Each shell company must be duly investigated, instead of a ‘name and shame’ data dump
The decision by the Ministry of Corporate Affairs to crack down on so-called ‘shell companies’, disqualify select directors in these entities and debar them from taking board positions for a specified period of time cannot be faulted. This would begin the clean-up of the Augean stables of firms set up in many cases with less than bona fide intent and having virtually no business operations. However, the Union government’s move to publicise the identities of some of these individuals with a view to ‘naming and shaming’ them is fraught with risk; the devil, as always, is in the detail. While the underlying motive for this action, as cited by the ministry, of “breaking the network of shell companies” in the government’s fight against black money is laudable, there is a real danger of inadvertently tainting genuine firms and individuals. This was in evidence when the Securities Appellate Tribunal recently gave relief to some entities over trading curbs hastily imposed on them by SEBI. Also, given the sheer scale of the task at hand, with the ministry identifying more than 1.06 lakh directors for disqualification, it is imperative that there be great care and diligence to ensure that the authorities do not penalise anyone who for non-mala fide reasons failed to comply with the relevant provisions of the Companies Act. After all, when the intention is to create “an atmosphere of confidence and faith in the system” as part of improving the climate for ease of doing business, the onus must be on taking to task only those who intend to subvert the law.
At a broader level, the Centre and the regulatory arms need to address the underlying systemic shortcomings that have allowed so many companies, both listed and unlisted, to become vehicles of malfeasance. For one, as so many entrepreneurs establishing medium, small or micro enterprises have found to their chagrin, it is far easier to register a firm than it is to dissolve or wind it up. Similarly, in the case of public limited companies, a major portion of the extralegal activities including price rigging of shares, insider trading and other questionable practices have been found to occur in the large mass of smaller companies. The problems of acute illiquidity, weak governance and regulatory oversight have combined with the difficulty in delisting to make these firms prime targets for financial fraudsters and money launderers. The solutions, therefore, need to be targeted at addressing the deep-rooted maladies rather than just the symptoms, making it easier for entrepreneurs to deregister and/or delist a company. The government has already shown it is prepared to act in terms of enacting the necessary legislation to address banking sector stress by adopting the Insolvency and Bankruptcy Code. A simplified process, possibly online, to dissolve or delist would usher in significant benefits, including improved governance, and ensure that all stakeholders from small retail investors to corporate promoters have an enabling atmosphere to operate freely by remaining compliant with the law or risk facing stringent penal action.
Date:21-09-17
States of the Opposition
Political parties must frame their campaign as a referendum not on leadership but on democratic values
G. Sampath
late, it’s become almost a matter of conventional wisdom that the 2019 Lok Sabha elections are the Bharatiya Janata Party’s for the taking. The only unknown, apparently, is the margin of victory. If the party’s ambitious ‘Mission 350-plus’ plan proves successful, we could soon have a Parliament that is practically ‘Opposition-mukt’.
In such a scenario, does it still make sense to hope for a meaningful Opposition in the run-up to 2019 and after? If yes, what might be the contours of a political strategy that would enable it to pose a credible challenge to the BJP juggernaut?
Reams have been written about the failures of the Opposition parties. Far from holding the government to account, they have either been dormant or busy fighting for survival. The BJP, on the other hand, has been steadily expanding its footprint. It was in power in five States before the 2014 polls. Today the National Democratic Alliance is in power in 18 out of the 29 States. Thirteen of those have a BJP Chief Minister.
Some have argued that the Indian polity has reverted to a state it has witnessed before — that of single-party dominance, with the BJP taking the place of the Congress. While this is true in a formal sense, there is a big difference in substantive terms, one that could seal the fate of Indian democracy as we have known it.
The Congress system
For more than two decades after Independence, political competition in Indian democracy took place within the confines of what political scientist Rajni Kothari termed ‘the Congress system’. It denoted a polity marked by single-party dominance. Until the onset of the ’70s, the Congress incorporated oppositional drives into itself by way of multiple factions at the regional and national level that mirrored the extraordinary pluralism and diversity of a complex nationhood.In a traditional society where a political culture centred on democracy was yet to strike roots, it was the accommodative pluralism of the ‘Congress system’ that allowed the normative modernity of the Constitution to slowly achieve a fragile social hegemony. More than the ‘steel frame’ of the bureaucracy, it was the elastic frame of the ‘Congress system’ that held the country together by respecting its pluralistic genotype.
Subsequently, as the Congress went into decline, regional configurations came to power in State after State, and India entered the coalition era. As it lost ground in State politics, the Congress was forced to play ball with smaller parties at the national level. Seen another way, the intra-party coalitions within the ‘Congress system’ became externalised into an inter-party dynamic in the coalition era that began with the ninth Lok Sabha in 1989, and continued till the 2014 elections.
Political competition being what it is, the vacuum at the national level caused by the shrinkage of the Congress has now been filled by the BJP. It did so by scripting an alternative national narrative around three elements: a Hindutva-infused nationalism; turning elections into a referendum on national leadership, specifically Narendra Modi’s leadership; and framing the electoral competition in all-India terms rather than engage with State-level issues.If the Opposition has floundered so far, it is because it has tried, without much conviction, to challenge the BJP on its narrative home ground. Not surprisingly, its attempts have failed to strike a chord.
Debating nationalism ends up giving more oxygen to chauvinism. The Opposition does lack a politician who can match Mr. Modi’s appeal. And regional leaders are better off sticking to State-level issues where they are on stronger political ground than trying to reinvent themselves overnight for a national role. In other words, the Opposition needs to stop being reactive and formulate its own counter-narrative.
Lessons from the past
Much has been made of the Congress being reduced to 44 seats in the Lok Sabha. It is taken as a sign of structural weakness in the Opposition camp. Yet, after Independence, in the first five Lok Sabhas, the highest number of seats held by an Opposition party was 44 seats. Did that mean India was ‘Opposition-mukt’ for a quarter of a century?History shows us that the Congress’s own fall from dominance was sparked by challenges at the State-level, not by a national rival. But that was possible because of the space for political pluralism offered by the ‘Congress system’.
The fundamental difference between the ‘Congress system’ and the ‘BJP system’ of one-party dominance is the latter’s determination to eliminate this pluralistic space. Politically, this is the toughest challenge facing the Opposition, as well as the biggest weakness of the BJP, one that could be tapped to construct an alternative narrative.Put simply, the Opposition’s counter-narrative would need to dwell on two aspects. One, it must convey that the 2019 polls are about choosing between two options: a coalition regime structurally constrained to protect the values of pluralism and federalism, and a stable majority under an authoritarian leadership unlikely to entertain democratic niceties.Second, the Opposition needs to frame the election as a referendum not on leadership but on democratic values. A massive win for the BJP in 2019 would certainly pose a threat to the historical consensus, established at the time of Independence, which institutionalised pluralism, a degree of federal autonomy, and a democratic framework for nation-building. The Opposition has the simple but onerous task of using its political imagination to bring this threat to the centre of the electoral agenda.
Onus on regional parties
Its political strategy, therefore, must aim for a hung Parliament and a coalition government. An ideal outcome would be one where no party gets more than 170-180 seats. A ‘Mission 180 minus’, as it were. With such numbers, even a BJP-led coalition government would be a victory for the Opposition, as the objective of safeguarding India’s pluralism would have been achieved.
Regional parties are best placed to take the lead here, for they are the ones which would be hardest hit by a creeping centralisation of power. If they could come together, with or without the Congress, over a single point agenda of protecting India’s pluralism, it would obviate the need for a formal pre-poll or seat-sharing arrangement. There is no other way that, say, a Trinamool Congress and a Communist Party of India (Marxist) would come together to battle a common rival that could prove more lethal to both than they have been to each other. Given that the BJP has always struggled more against non-Congress, regional opponents, it is also a more canny electoral strategy.And in case they still lose badly, they can take heart from the fact that India’s political traditions give the Opposition an institutional role disproportionate to their actual numbers in Parliament, through mandatory membership of key committees, appointments panels, and so on. So, regardless of how they fare in 2019, Opposition parties would continue to have a major role to play.
All said and done, Indian democracy has never fared well under powerful parliamentary majorities led by a charismatic Prime Minister unchecked by coalition dynamics. We have two examples, in Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. While one briefly downed the shutters on democracy, the other gave a fillip to Hindu fundamentalism and tried to muzzle the press.The Opposition’s success would ultimately hinge on how effective it is in convincing the people that if they value their nation’s democratic traditions as much as they do development, they must either elect a coalition government in 2019, or force the ‘BJP system’ to become more like the ‘Congress system’, not by importing Congressmen, but by imbibing the values of pluralism and respect for dissent that the Congress stands for in its Nehruvian vision of itself, if not always in reality.
उम्र के इस मोड़ को चाहिए जीने के नए मुकाम
ऋतु सारस्वत, समाजशास्त्री (ये लेखक के अपने विचार हैं)
देश के लगभग आधे लोग अपने बच्चों के भरोसे ही काम से रिटायर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की हाउस होल्ड फाइनेंस समिति ने कहा है कि इससे देश की युवा पीढ़ी पर काम का अनावश्यक दबाव पड़ता है, साथ ही दो पीढ़ियों के रिश्तों में भी तनाव बढ़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 77 प्रतिशत लोग या तो इस बात की कल्पना ही नहीं करते कि वे रिटायर होंगे, न रिटायरमेंट की कोई योजना बनाते हैं। लगातार ऐसे अध्ययन सामने आ रहे हैं, जो बुजुर्गों की खराब स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। हेल्पेज इंडिया की ओर से किए गए सर्वे भी बता रहा है कि घर से लेकर बाहर तक बुजुर्र्गों को असम्माननीय व्यवहार का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ दशकों में कई बार इस संबंध में चिंताएं भी जाहिर की गई हैं। ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007’ का प्रावधान, बुजुर्गों को कानूनी ढाल देता तो है, लेकिन भारतीय अभिभावक न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से हिचकते हैं, क्योंकि इसे वे अपने परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच के रूप में देखते हैं।
भारत ही नहीं, दुनिया भर में बुजुर्गों की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए जरूरी है कि बड़े स्तर पर इसके निराकरण के मार्ग ढूंढे़ जाएं। हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि समाज परिवर्तनशील होता है। चाहे-अनचाहे भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जो परिवर्तन हुए हैं, उन्होंने बुजुर्गों को असहायता और अकेलापन दिया हैै। इसका एक मुख्य कारण आर्थिक निर्भरता है, जो उनके आत्मविश्वास को तोड़ती है और भावनात्मक रूप से उन्हें कमजोर बना देती है। ‘बच्चों को बुढ़ापे की लाठी’ मानने की मानसिकता का त्याग अब जरूरी हो गया है, लेकिन समाज में कोई वैकल्पिक सोच उपलब्ध नहीं है। यकीनन बच्चों की उन्नति और शिक्षा का दायित्व अभिभावकों का है, लेकिन उसके लिए अपनी सारी जमा-पूंजी लगा देना, उचित नहीं। यह जरूरी है कि अपनी आय का एक निश्चित अनुपात वृद्धावस्था के लिए बचाना चाहिए। आर्थिक सबलीकरण, सुखद वृद्धावस्था की पहली शर्त है, लेकिन जहां गरीब ही नहीं, निम्न मध्यवर्ग तक के लोग बमुश्किल गुजारा करने लायक कमा पाते हों, वहां यह काम बहुत आसान भी नहीं है।
आंद्रे नारुआ ने कहा है कि ‘व्यस्त आदमी को बूढ़ा होने की फुर्सत ही नहीं’ मिलती। सच भी यही है, पर यह तब तक संभव नहीं है, जब तक कि व्यस्तता का पैमाना वृद्धों के लिए बच्चों व घर की चारदीवारी के भीतर तक हो। घर के बाहर अपने हमउम्र साथियों के बीच रहना, अपने उन सपनों को पूरा करना है, जो जीवन की आपाधापी में कहीं पीछे छूट गए, यही साथ उनके जीवन में रंग भर देता है। सामाजिक सरोकार से जोड़ने का प्रयास एकाकीपन को दूर करने का बेहतर रास्ता है। एकाकी परिवार, भारतीय समाज का अब सच बन चुके हैं। एक या दो बच्चों के बीच अपनी खुशियां तलाशने की कोशिश पारिवारिक उलझनों को पैदा करती है। समाज को अगर युवाओं की ऊर्जा की आवश्यकता है, तो बुजुर्गों के अनुभवों की भी उतनी ही जरूरत है। अपने हमउम्र साथियों के साथ समय बिताना और उन लोगों से जुड़ना, जिनके अपने बाहर रहते हैं या है ही नहीं, जीवन को एक नई परिभाषा देगा। ‘ओल्ड एज होम’ को अभिशाप मानने की बजाय एक नई परिपाटी शुरू की जा सकती है। ‘फ्रेंड्स होम’ आर्थिक विवशताओं और दुव्र्यवहारों के लिए नहीं, बल्कि अपने हमउम्र साथियोंके साथ रहने की चाह के कारण अस्तित्व में लाए जाएं। ये आश्रय वृद्धावस्था को सहजता से भर सकते हैं।इसकी एक बानगी छत्तीसगढ़ के रायपुर में देखी जा सकती है, जहां 700 युवा अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपतियों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं। उनकी चिकित्सा सुविधा से लेकर अन्य कामों में भी उनकी सहायता करते हैं। ये वे बुजुर्ग हैं, जिनके बच्चे नौकरी या बिजनेस के चलते विदेश या देश के अलग-अलग हिस्सों में शिफ्ट हो गए हैं और ऐसा कोई करीबी व्यक्ति भी नहीं है, जो उनकी देखभाल कर सके। वृद्धावस्था कोई बीमारी नहीं है, जीवन का एक पड़ाव है और यह पड़ाव तभी सुखद हो सकता है, जब हम इसके लिए खुद को तैयार करें। साथ ही इस सच को भी स्वीकारें कि संयुक्त परिवार का दौर अब नहीं लौट सकता।
हर हाल में हो दुरुस्त
के.सी. त्यागी
नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक स्वास्य व्यवस्था में एक अभुतपूर्व बदलाव की सिफारिश के तहत स्वास्य सेवा को निजी हाथों में देने की बात कही गई है। पिछले माह घोषित इस योजना के अंतर्गत ‘‘पीपीपी’ यानी पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप के तहत जिला स्तरीय सार्वजनिक अस्पतालों व स्वास्य केंद्रों को निजी संस्थानों के साथ सम्बद्ध किया जाना प्रस्तावित है। गैर-संचारी रोगों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से इस मॉडल अनुबंध का प्रस्ताव नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। प्रस्तावित मॉडल के तहत जिला अस्पताल की इमारतों में निजी अस्पतालों को 30 वर्षो के लिए पट्टे पर जगह व अन्य व्यवस्था मुहैया कराने और देश के आठ बड़े महानगरों को छोड़कर अन्य शहरों में 50 से 100 बेड वाले अस्पताल बनाने के लिए जमीन प्रदान करने की अनुमति दी गई है।
निजी निवेशकों को आकर्षित करने के क्रम में आयोग द्वारा अस्पताल परिसर के 60,000 वर्ग फीट जमीन प्राइवेट संस्थान को देने का प्रस्ताव भी है। शर्त है कि जिन जिला अस्पतालों में प्रतिदिन एक हजार से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं; केवल उन्हीं अस्पतालों में निजी व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इस प्रस्ताव को लेकर नीति आयोग की दलील है कि नई नीति के लागू हो जाने से हृदय संबंधी, कैंसर और श्वास रोगों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। सच है कि देश में गंभीर बीमारियों की वजह से होने वाली मौत में लगभग 35 फीसद भागीदारी इन्हीं तीन बीमारियों की है। आयोग की सिफारिश को रोग उन्मूलन की दृष्टि से देखे जाने पर स्पष्ट है कि सरकार लचर पड़ी चिकित्सा व्यवस्था को बल देना चाहती है। इससे इतर दूसरा और मजबूत पक्ष यह भी है कि क्या व्यवस्था के निजीकरण मात्र से आम जनमानस को अपेक्षित लाभ मिल पाएगा? सवाल यह भी है कि जब पूर्णत: सरकारी तंत्रों की निगरानी में कैंसर, हृदय रोग और श्वास रोग आदि पर काबू नहीं पाया जा सका तो क्या गारंटी है कि निजी संस्थानों से सम्बद्धता के बाद मरीजों को सुविधाजनक एवं सस्ता उपचार मिलना शुरू हो जाएगा? यह पहली बार नहीं जब नीति आयोग की ओर से निजीकरण के संकेत मिले हैं। सर्वप्रथम 2015 में आयोग द्वारा स्वास्य क्षेत्र में निजी निवेशकों और बीमा कंपनियों को मुख्य भूमिका में लाए जाने की कवायद शुरू हो गई थी। इसी दौरान सार्वजनिक चिकित्सा के खर्चो में कटौती करने और इस क्षेत्र में हो रहे निवेश पर काबू पाने और सार्वजनिक स्वास्य सुविधा के तहत मरीजों को निशुल्क मिल रही दवाइयों व अन्य सेवाओं को नियंत्रित करने की भी अनुशंसा की गई थी। हालांकि मंत्रालय द्वारा इस दिशा में अब तक बदलाव की घोषणा नहीं हुई है लेकिन निजीकरण की ओर बढ़ती प्रक्रिया से खासकर गरीब जनसंख्या में अविास का संचार जरूर हुआ है। चिंता है कि निजीकरण का असर उनकी प्राथमिक चिकित्सा को प्रभावित न कर दे। निजीकरण की स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि सरकार पीपीपी मॉडल का संचालन किसके जिम्मे छोड़ेगी? निवेशकों की हिस्सेदारी की स्थिति में निश्चित रूप से उनका भी दबदबा होगा। नीति निर्माण से लेकर, मरीजों से बर्ताव और प्राइवेट डॉक्टरों की मनमानी आमजनों की चिंता के मुख्य बिंदु हैं।
वर्तमान व्यवस्था में सरकारी डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरतने, अनुपलब्धता और इलाज को मना किए जाने तक की बात सामने आती रहती है। नई प्रस्तावित व्यवस्था में राहतपूर्ण यह है कि गंभीर हालत के मरीजों को सार्वजनिक अस्पताल परिसरों से परिचालित निजी अस्पतालों में त्वरित देख-भाल के लिए भेजा जा सकता है। इसके लिए चिकित्सा अधीक्षक की अनुमति का प्रावधान है। इसी माह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना न सिर्फ सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा है बल्कि यह देश भर के सरकारी-प्राइवेट अस्पतालों के लिए आईना भी है। समय-समय पर इस तरह की घटनाएं सरकारी तंत्रों की पोल खोलती रहती हैं। हैरानी है कि भारत पहले से ही स्वास्य क्षेत्र पर सबसे कम खर्च करने वाला राष्ट्र है। कुल जीडीपी का मात्र एक फीसदी हिस्सा देश के सार्वजनिक स्वास्य पर खर्च किया जाता है जो नियंतण्र सूची में निम्नतम है। विकसित राष्ट्रों में यह आंकड़ा लगभग 10 गुना ज्यादा है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2012 से 2017 के दौरान सरकारी खर्चे में कटौती की गई है। वर्ष 2014-15 के स्वास्य बजट में 5100 करोड़ की कटौती हुई। इस बार सांकेतिक बढ़ोतरी जरूर हुई लेकिन वर्तमान चुनौतियों से लड़ने में नाकाफी है। नये बजट में वर्ष 2017 तक कालाजार और फलेरिया, वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग एवं 2020 तक खसरा एवं 2025 तक टीबी से देश को मुक्ति दिलाने की घोषणा निश्चित रूप से उत्साहवर्धक है लेकिन विश्व स्वास्य संगठन के एक मूल्यांकन के अनुसार भारत को टीबी मुक्त होने में 2050 तक का समय लग सकता है। दो विासपात्र स्रेतों के भिन्न मतों से संशय होना भी लाजिमी है। पिछले कुछ वर्षो में तमाम सुख-सुविधाओं से लैस हजारों की संख्या में बड़े आधुनिक अस्पताल खोले गए हैं लेकिन महंगे इलाज के कारण इन अस्पतालों से भारतीय जनसंख्या के बड़े हिस्से को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में संपन्न और आम नागरिकों के इलाज के बीच एक बड़ी खाई बन गई है। स्वास्य बीमा भारतीय संरचना के अनुकूल नहीं है। एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक आबादी के पास न तो कोई सरकारी स्वास्य स्कीम है और न ही कोई निजी बीमा। इस दुर्दशा में निजीकरण के बजाय वर्तमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ज्यादा कारगर हो सकता है। सार्वजनिक स्वास्य के लिए अधिक बजट का प्रावधान, अनियमितता के प्रति कड़ी निगरानी, आधारभूत संरचना का विकास, जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा आदि बीमार पड़ी चिकित्सा व्यवस्था को पुन: दुरुस्त कर सकता है।(लेखक जद (यू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)
