
21-07-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.

Date: 21-07-25
The New Buzz
Unregistered drones are law enforcement’s new challenge, one that’s not easily solved
ET Editorials
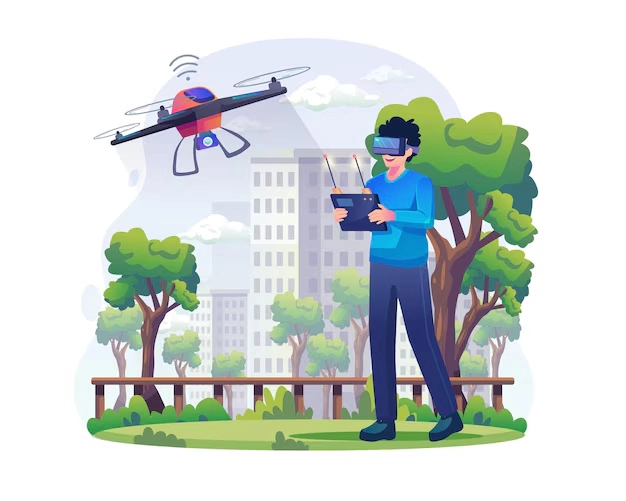
Civilian drones are proving to be a new headache for law enforcement across the country- an unsurprising fallout of drones becoming cheaper and more widely available. In towns and villages in western UP, for example, drones are regularly spotted after sundown. With growing suspicions that these are linked to local thefts or dodgy characters looking to make privacy- violating videos, people have been forced to mount rooftop vigils. Complaints of videography and snooping using drones, especially in relation to sensitive govt facilities, have been growing in Tamil Nadu. Other state authorities too are seized of the matter.
There are three issues here. First, compliance and enforcement of drone regulations are weak. To operate a civilian drone in India one needs to register the drone on the DGCA website, obtain a remote pilot licence, and be aware of flying regulations, including locations of no-fly zones. But most private drone operators don’t bother, and there are now lakhs of unregistered drones. As of April this year, only 32,000 were registered against an estimated 5L-plus drones in the country.
Second, despite the fact that import of drones is banned in India, foreign drones – especially of illegal Chinese make – are found across grey markets throughout the country. Chinese drones are actually smuggled across India’s porous borders. They are dismantled for the journey before being reassembled here. Third, given the rise of the attention economy, drone videos that infringe privacy are in high demand.
The sheer number of drones is seriously stretching limited police resources. One solution is faster development of the Indian drone industry to lower domestic drone prices. This will stem imports, and perhaps ensure better monitoring of drone use. But it’s not a guarantee by any means. Drones are going the way of all tech breakthroughs- the baddies will more often than not outsmart the good guys.
Date: 21-07-25
A long list
The designation of TRF as a terror group should put more pressure on Pakistan
Editorials
The decision of the U.S. to designate The Resistance Front (TRF) group that claimed responsibility for the Pahalgam terror attack in April 2025, as a Foreign Terrorist Organization (FTO) and a Specially Designated Global Terrorist is a development that should undergird the global fight against terror. The Ministry of External Affairs has called it “a timely and important step”. For one, the U.S. State Department has acknowledged the severity of the Pahalgam attack. It also names the TRF as a “front and proxy” for the Lashkar-e-Taiba (LeT), which Pakistan claims it has rendered “defunct”. Even though the U.S. added groups such as the LeT and the Jaish-e-Mohammad to its FTO list in 2001, they have masterminded attacks in India since then. The U.S. has also partially made amends for the TRF’s name having been kept out of the UN Security Council (UNSC) resolution condemning the Pahalgam attack, apparently at Pakistan’s behest, but with the concurrence of the U.S. and other P-5 members. It is hoped that the designation will now help India’s case in designating the TRF at the UNSC, under the 1267 Committee for sanctions, also strengthening the trans-national legal pursuit of those behind the attack.
While this is a positive step, it is necessary to put the Trump’s administration’s other actions since the Pahalgam attack into perspective. After India launched Operation Sindoor, the U.S. has countered India’s narrative on the four-day conflict on several occasions. Mr. Trump, as well as Secretary of State Marco Rubio, have repeatedly made the claim that the U.S. negotiated the India- Pakistan ceasefire, and averted a nuclear conflict by using trade ties as leverage – an equivalence which Pakistan has been happy to endorse. Mr. Trump’s unprecedented White House lunch and praise for the Pakistan military chief, Field Marshal Asim Munir, came hours after the government had said that Prime Minister Narendra Modi had cleared the picture with Mr. Trump, and brings into question just how much pressure the U.S. is willing to put on Pakistan to act against terrorism. The Trump administration had held out the promise of doing more to support India in its fight against terrorism by fast-tracking the extradition, in April, of Tahawwur Hussain Rana, who was wanted by India for the 2008 Mumbai attacks. It is hoped that the TRF’s listing means that the U.S. is recommitting to that objective. Given that the real challenge lies more in credibly ending Pakistan’s support to these groups, New Delhi must focus on its efforts, diplomatic as well as legal, to ensure justice for the victims and to prevent further terrorist acts.
Date: 21-07-25
विश्व के लिए खतरनाक होगा टैरिफ का दांव
शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं )
खातिर गजनवी की मशहूर गजल का मतला है-गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। पुतिन और ट्रंप के बीच हाल में कुछ ऐसा ही हुआ है। हां, बात केवल इतनी ही नहीं है। 2013 की मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतिस्पर्धा को लेकर मास्को गए ट्रंप ने रूसी अरबपतियों और राष्ट्रपति पुतिन की खातिरदारी से अभिभूत होकर कहा था कि वे राष्ट्रपति ओबामा से भी अधिक प्रभावशाली हो चुके हैं पुतिन का रंग उन पर इतना गहरा चढ़ा कि राष्ट्रपति बनने के बाद 2018 के हेलसिंकी शिखर सम्मेलन में उन्होंने अपने खुफिया तंत्र के खिलाफ पुतिन का पक्ष लेते हुए यह मानने से इन्कार कर दिया कि रूस ने अमेरिकी चुनाव में गड़बड़ी कराई थी। पुतिन के साथ अपने खास रिश्ते का दम भरते हुए उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति बनने के 24 घंटों के भीतर युद्धविराम करा देंगे। जब वह नहीं हुआ तो उन्होंने रूस के प्रतिबंध हटाने और क्रीमिया को रूस के भाग के रूप में मान्यता देने जैसे प्रलोभन देकर पुतिन को मनाने की कोशिशें कीं । जंग का ठीकरा जेलेंस्की के सिर फोड़ा, उन्हें तानाशाह बताते हुए व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने बुरा-भला कहा। उन्होंने यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक मदद रोक ली और बिना शर्त बातचीत के लिए राजी किया।
युद्ध विराम के लिए ट्रंप ने पुतिन के साथ छह बार फोन वार्ताएं कीं, परंतु पुतिन न केवल बात लटकाते रहे, बल्कि हर बातचीत के बाद बड़े-बड़े हमले करते रहे। इस महीने की बातचीत के बाद ट्रंप का पुतिन से मोहभंग हो गया और उन्होंने कहना शुरू किया कि वे उनसे नाखुश हैं। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वे पुतिन से निराश हैं, पर हताश नहीं। उन्होंने यूक्रेन को नाटो के माध्यम से अधुनातन रक्षा प्रणाली और मिसाइलें देना शुरू करने का एलान किया और पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे 50 दिनों के भीतर युद्ध विराम के लिए राजी नहीं हुए तो रूसी माल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ जैसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। नाटो महासचिव मार्क रूटा ने तो चीन, भारत और ब्राजील को सीधे ही कह दिया कि या तो तीनों मिलकर पुतिन को युद्ध विराम के लिए राजी करें, अन्यथा अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए तैयार हो जाएं। यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं और अमेरिकी सीनेट रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने वाले प्रस्ताव की तैयारी कर रही है।
रूस प्रतिदिन लगभग 70 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है, जिसका 47 प्रतिशत चीन खरीदता है और 38 प्रतिशत भारत । रूस इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। उसके तेल की बिक्री बंद होने से दुनिया में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर चीन और भारत पर तो पड़ेगा ही, यूरोप और अमेरिका भी उससे अछूते नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई बढ़ेगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। इससे रूस का नुकसान तो तब होगा जब चीन, भारत और ब्राजील तेल खरीदना बंद करेंगे। हालांकि तेल की कीमतें बढ़ने से रूस को फायदा होना तुरंत शुरू हो गया है। वैसे भी पुतिन को लगता है कि ट्रंप की धमकी गीदड़ भभकी के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए पुतिन ने यूक्रेन पर 700 ड्रोन और दर्जन भर मिसाइलों से बड़ा हमला किया। अमेरिकी चेतावनी के जवाब में रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जखारोवा ने भी कहा कि अल्टीमेटम, ब्लैकमेल और धमकियां हमें मंजूर नहीं हैं। हम अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। रूसी शेयर बाजार में भी घबराहट की जगह तेजी दिखाई दी।
ट्रंप का पुतिन से मोहभंग होना तो समझ में आता है, परंतु आर्थिक प्रतिबंधों के जिस हथियार से बाइडन कुछ हासिल नहीं कर पाए तो उसी को दोबारा चलाने का मकसद क्या हो सकता है? सुप्रसिद्ध इतिहासकार युवाल नौआ हरारी के अनुसार ट्रंप किलेबंदी की मानसिकता से काम करते हैं। उनकी नीतियों में किसी न किसी ठोस प्राप्ति का स्वार्थं छिपा रहता है। यूक्रेन की सैनिक मदद के लिए उन्होंने नाटो को माध्यम बनाया ताकि यूक्रेन को हथियार मिल जाएं और उन्हें नाटी के जरिये उनके दाम । ट्रंप दवा कर चुके हैं कि चीन के साथ सैद्धांतिक रूप से व्यापार सौदा हो चुका है, परंतु उस दावे को तीन हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन सौदे पर मुहर नहीं लग पाई है। उन्होंने भारत के साथ भी सौदा हो जाने का संकेत दिया है। अलबत्ता औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है। हो सकता है कि इन्हीं व्यापार सौदों को मनमुताबिक और जल्दी निपटाने के लिए रूसी तेल खरीदने वालों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी जा रही हो। वरना यह बात पुतिन भी जानते हैं और ट्रंप भी कि शी चिनफिंग भी ट्रंप की धमकी में आकर रूस से तेल लेना बंद नहीं करने वाले। वे टैरिफ जंग में भी नहीं झुके, क्योंकि चीन के पास दुर्लभ खनिजों, चुंबकों और सेमीकंडक्टरों का ब्रह्मास्त्र था। उसके साथ आखिरकार ट्रंप को ही सौदा पटाना पड़ा।
ट्रंप समझ चुके हैं कि सवा लाख से अधिक सैनिकों और अर्थव्यवस्था की बलि चढ़ा चुके पुतिन को बातों और धमकियों से पीछे हटाना संभव नहीं हैं। न ही वे इस अंतहीन लड़ाई में यूक्रेन के लिए अमेरिकी खजाना खोलने की तैयार हैं। इसलिए उन्होंने नाटो के जरिये हथियार बेचने का रास्ता चुना है, ताकि यूक्रेन अपनी रक्षा करते हुए रूसी सेना और रक्षा तंत्र को इतनी चोट पहुंचाता रहे कि एक दिन पुतिन थककर बातचीत के लिए विवश हो जाएं। दूसरी ओर पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन की सैनिक और खुफिया शक्ति और रक्षा उद्योग को तबाह कर उसे ऐसे नाकाम राज्य में बदल देना है जहां रूसी हमलों के भय से कोई निवेश न करे और वह रूस पर आश्रित होकर रह जाए। इस खेल में भारत को कूटनीतिक निपुणता के साथ चीन के साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि ट्रंप उसी की सुनते हैं जिसके पास पलटवार की क्षमता होती है। चीन के पास पलटवार के लिए दुर्लभ खनिज हैं और रूस के पास तेल और अनाज । ऐसे में भारत को अपनी कूटनीति पर दांव लगन होगा।

Date: 21-07-25
अमेरिका की नीतियों की नकल खतरनाक
मिहिर शर्मा
भले ही आने वाले दशकों में अमेरिका की आर्थिक और सैन्य शक्ति कमजोर हो जाए, लेकिन उसकी सांस्कृतिक मजबूती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तमाम महाशक्तियों के साथ अक्सर ऐसा ही होता आया है। समय के साथ उनकी अर्थव्यवस्थाओं के शिथिल पड़ने के बावजूद विचारों और संस्कृति की दुनिया में उनकी धमक लंबे समय तक सुनाई देती है। आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका 1880 के दशक में ही ब्रिटेन से अधिक ताकतवर बन गया था लेकिन उसकी वैचारिक-सांस्कृतिक जमीन को मजबूत होने में 40-50 साल और लग गए। और इस बीच अस्तित्व में आया हॉलीवुड |
वैचारिक ताकत का तात्पर्य केवल फिल्मों और संगीत से नहीं है। किसी महाशक्ति की आंतरिक क्रियाशीलता कैसे शेष दुनिया पर असर डालती है, इसका पता उस देश की आंतरिक राजनीतिक बहसों से चलता है। किसी न किसी रूप में ये बहसें धुरी का काम करती हैं जिसके इर्द-गिर्द अन्य देशों की राजनीति घूमती दिखाई देती है।
अमेरिकी राजनीति ने भिन्न सामाजिक और आर्थिक ढांचे वाले देशों को किस तरह प्रभावित किया है, इस पर एक नजर डालते हैं । अमेरिका में नस्लीय उत्पीड़न का ऐसा कड़वा इतिहास रहा है, जिसकी नजीर दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती । ब्राजील जैसे कुछ अन्य देश भी आंशिक रूप से दास व्यापार प्रथा द्वारा निर्मित हुए थे और वहां भी कानूनी तौर पर गुलामी की प्रथा उतनी ही पुरानी थी जितनी अमेरिका में, या शायद उससे भी पुरानी ।
लेकिन अमेरिका में जैसी दासता, संवैधानिक नागरिक अधिकार और पीढ़ियों से चली आ रही नस्लीय अलगाव की स्थिति रही वैसा और कहीं नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी राजनीति जिस प्रकार इन मसलों से निपटती है अथवा उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब अमेरिका में ‘ब्लैक लाइव्स मैटर्स’ विरोध-प्रदर्शनों या व्यापक स्तर पर युवा हिस्पैनिक पुरुषों (लैटिन अमेरिकी देशों के स्पैनिश भाषी लोग ) के डॉनल्ड ट्रंप का समर्थन करने जैसे नस्लीय आक्रोश फूटते हैं तो यह एक बेचैन समाज में उभरती बहुत ही अलग तरह की नस्लीय सहमति का रूप सामने आता है। जातीय या नस्लीय तनाव से जूझते अन्य देश इससे बहुत सीख नहीं ले सकते। यूरोप में नस्लीय अल्पसंख्यकों का अफ्रीकी-अमेरिकियों से एकदम अलग इतिहास रहा है। वहीं भारत में भी जातिगत भेदभाव है, जिसकी तुलना अक्सर नस्लीय उत्पीड़न से की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सफल हिंदुत्व एजेंडा दिखाता है कि एक अलग तरीके से इसे कैसे राजनीति के लिए अपने पक्ष में किया जा सकता है। अमेरिका की नस्लीय राजनीति से दुनिया के अन्य देश कुछ सीख तो सकते हैं, लेकिन उन्हें यह याद रखना होगा कि इसमें से कुछ भी उनके लिए प्रासंगिक नहीं है। वे इन नीतियों को अपने यहां लागू नहीं कर सकते।
एक और चीज जो अमेरिका को खास बनाती है, वह है अपनी सरकार की भूमिका के प्रति उसका नजरिया । कहा जाता है कि अमेरिकी लोग छोटी सरकार को पसंद करते हैं। कुछ हद तक यह सही भी है। अमेरिका में सरकारी खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 36 फीसदी है, जबकि जापान में यह 41 फीसदी और स्वीडन में 47 फीसदी तक है। लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका में बजटीय सीमा जैसी कोई अवधारणा नहीं है। सेंट लुइस के फेडरल रिजर्व बैंक के अनुसार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में इसकी संघीय सरकार का घाटा 6.3 फीसदी है। ट्रंप सरकार का नया बजट विधेयक ऋण को बढ़ने से रोकने की कोई वास्तविक योजना सामने नहीं रखता, जिससे यह बोझ बढ़ता जा रहा है।
लंबे और मजबूत वित्तीय इतिहास वाली अर्थव्यवस्था के मालिक ब्रिटेन समेत कोई भी देश ऐसी आर्थिक अनियमितता से बच नहीं सकता। फिर भी ऐसा माना जाता है कि औद्योगिक नीति से लेकर विनियमन और पूंजीगत लाभ कर तक अमेरिका की आर्थिक बहसों और धारणाओं का शेष विश्व की आर्थिक नीतियों पर असर पड़ता है। क्या अन्य देश वास्तव में इससे प्रभावित होते हैं। यहां तक कि उस समय भी जब लोक वित्त में सबसे महत्त्वपूर्ण बाधा मानी जाने वाली सरकार की बजट सीमा उन पर लागू नहीं होती।
यह उम्मीद करना बेहद खतरनाक होगा कि कोई भी देश अमेरिका की सब्सिडी, व्यापार नीति, शोध, कर संरचना या उसकी नियामकीय बहसों से कोई नीतिगत सबक सीख सकता है या उन्हें अपने यहां लागू कर सकता है। क्योंकि सभी किसी न किसी तरह इस तथ्य से वाकिफ हैं कि अमेरिका वित्तीय बाजारों से बेखटके असीमित मात्रा में धन उधार ले सकता है जबकि कोई अन्य देश ऐसा नहीं कर सकता। हम सभी अमेरिका, वहां की राजनीति व नीतियों से प्रभावित हैं और दशकों तक रहेंगे भी, लेकिन यह केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में हो, प्रतिभागी या शिष्य के रूप में ऐसा कतई न करें।
Date: 21-07-25
आर्थिक नीति और विकास की राह
सुरेश सेठ

आर्थिक नीति के क्रियान्वयन से ही विकास नीति बनती है। समय-समय पर आर्थिक दरों की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से की जाती है, जिसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। रिजर्व बैंक पहले नीति की घोषणा करता था, अब सहयोग और परामर्श के लिए एक मौद्रिक समिति भी बन गई है। हर मौद्रिक नीति का आदर्श यही होता है कि एक ओर वह महंगाई पर नियंत्रण रखे, दूसरी ओर देश के विकास में भी कोई बाधा न आए। हालांकि, सरकार के दावों में यही कहा जाता है कि महंगाई पर नियंत्रण पा लिया गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार, सुरक्षित महंगाई की दर चार फीसद है और इस वर्ष सूचकांक के आंकड़ों के मुताबिक यह 4.6 फीसद रही। अब इसके चार फीसद से भी नीचे आ जाने की संभावना है। वहीं इससे संबंधित घोषणाओं की ओर देखें, तो भारत दस वर्ष में दुनिया की ग्यारहवीं आर्थिक शक्ति से ऊपर उठ कर पांचवीं आर्थिक शक्ति बन चुका है। इस साल के अंत तक देश के चौथी आर्थिक शक्ति और दो वर्षों में तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की उम्मीद की जा रही है। अगर यह संभव हुआ तो इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। बार-बार यह घोषणा की जाती है कि भारत की विकास दर दुनिया के सभी देशों की विकास दर से अधिक है। मगर आम आदमी की हालत देखिए। जब वह बाजार में जाता है तो वस्तुओं की कीमतें कहती हैं, हमें हाथ न लगाओ।
जहां तक विकास दर का संबंध है, तो विकास किसका हो रहा है? देश की तीन-चौथाई आबादी तो जीवन के उसी स्तर पर खड़ी है, जिसे भुखमरी से उबारने के लिए अनुकंपा कहा जाता है। तरक्की के साथ- साथ अनुकंपा और रियायती संस्कृति की समय सीमा भी बढ़ती जा रही है। हम वर्ष 2047 में भारत को दुनिया का सिरमौर देश बना देना चाहते हैं। सांस्कृतिक लिहाज से हमारे गर्व का कोई अंत नहीं। हम बनना चाहते हैं विश्व गुरु, लेकिन नैतिक मूल्यों के पतन का यह हाल है कि जिस तरह की घटनाएं हमारे समाज में घट रही हैं, वह एक मूल्यहीन एवं पतनशील समाज का द्योतक हैं। खुशहाली सूचकांक को ही देख लीजिए, भारत इसमें कहीं पीछे है। एशिया में भी आम लोगों की खुशहाली हमारे पड़ोसी देशों में हमसे कहीं अधिक है। तो यह कैसा विकास है, कैसी तरक्की है, जिस पर हम फूले नहीं समा रहे ।
इसी तरक्की और विकास का अगला चरण प्राप्त करने के लिए पहल जारी है। आरबीआइ के गवर्नर ने कहा है कि मौद्रिक नीति ऐसी होनी चाहिए, जिसमें महंगाई पर नियंत्रण हो और सतत् विकास को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि ये दोनों पक्ष किसी देश की संतुलित आर्थिक नीति के लिए आवश्यक है। मगर आजकल चर्चा यह हो रही है कि भारत ने महंगाई पर काबू पा लिया है और बाजारों में मुद्रास्फीति उस दर पर आ गई है, जिसे रिजर्व बैंक सुरक्षित दर कहता है। नए आंकड़ों के मुताबिक, सुरक्षित दर 4.6 फीसद है, लेकिन अगले वर्ष इसके तीन फीसद तक हो जाने की उम्मीद है। मगर आम जनता को यह बात क्यों केवल घोषणाओं का अलंकार लगती है ? कहा जाता है कि मुद्रास्फीति पर हमने इसलिए नियंत्रण कर लिया है, क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हो गई हैं। वैसे तो किसी भी विकासशील देश का मुद्रास्फीति सूचकांक केवल खाद्य पदार्थों की कीमतों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसमें उसके बराबर का महत्त्व पूंजीगत निवेश और वस्तुओं को भी मिलना चाहिए। जैसा कि हमारे सूचकांक में नहीं है। इसी प्रकार, विकास दर को मापते हुए यह भी देखना चाहिए कि यह विकास देश के किस वर्ग का हो रहा है। क्या सारा विकास चुनिंदा निजी पूंजीपति वर्ग के पास ही जा रहा है ? जो बहुमंजिला इमारतों और महंगी गाड़ियों की सूरत में महानगरों में नजर आता है। आम आदमी आज भी रियायती दुकानों के बाहर कतार लगाए क्यों खड़ा है ? संविधान में ‘समाजवाद’ का शब्द रहे या न रहे, इस पर बहस से कहीं ज्यादा जरूरी है कि अमीर और गरीब के जीवन स्तर में अंतर कम से कम हो। नौजवानों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार की गारंटी मिले। इस समय देश में जनता को भूख से न मरने देने की गारंटी है, लेकिन उनके उचित पोषण की गारंटी क्यों नहीं है? क्यों देश में एक कुपोषित समाज आज भी मौजूद है। दुखद ये कि नई पीढ़ी कमजोर पैदा हो रही है और औसत उम्र विकसित देशों की तरह बढ़ नहीं रही है।
ऐसे में मौद्रिक नीति के उस आकलन की चर्चा होनी चाहिए, जो इन दिनों सुनाई पड़ती है। आमतौर पर यह समझा जा रहा था कि जब मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर लिया है और महंगाई दर चार फीसद पर आ गई है, तो रेपो रेट और घटा देना चाहिए। ब्याज दर और घटा देनी चाहिए, कर्ज सस्ता कर मासिक किस्तें भी कम कर देनी चाहिए, ताकि लोग नया निवेश करके देश को विकास की राह पर तेजी से ले जा सकें, लेकिन इसका क्या लाभ? अभी पिछली दो बार रेपो रेट को घटा कर एक फीसद कम कर दिया गया, जिससे इस वर्ष की शुरुआत से बैंकों में पर्याप्त नकदी हो गई है। अनुमान है कि 5.6 लाख करोड़ रुपए का टिकाऊ वित्तपोषण बैंकों को मिला है। क्या यह वित्तपोषण पूंजीगत निवेश की ओर गया है? जवाब है, नहीं। जो कर्ज दिए जा रहे हैं, उसका एक बड़ा भाग दिखाऊ उपभोग पर खर्च हो रहा है।
जब पूंजीगत विकास की दरों को देखते हैं, तो उसमें वह तरक्की नहीं पाते जो होनी चाहिए। 6.50 फीसद की विकास दर हमें 2047 तक दुनिया का सिरमौर देश नहीं बना सकती है ? इसके लिए कम से कम दस फीसद विकास दर चाहिए और पूंजी क्षेत्र में निवेश का कायाकल्प हो। इसके साथ ही लघु, मध्यम और सहकारी उद्योगों का भी विकास हो, ताकि हर वर्ष बेरोजगार होते नौजवानों की खेप को तत्काल रोजगार मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए जिस सही विकास नीति की तलाश हमें करनी है, उसमें इस बात का ध्यान देना होगा कि बातें केवल दावों या घोषणाओं के स्तर तक सीमित न रहे, बल्कि आम आदमी के जीवन तक जाएं।
आरबीआइ के गवर्नर ने भी कहा है कि एक और रेपो रेट को घटाना है या नहीं, इसका फैसला सोच-समझ कर किया जाएगा । कटौती का असर अभी शुरुआती दौर में है। जून में आधा फीसद तक कटौती की गई थी, लेकिन कुल एक फीसद कटौती के मुकाबले एक फीसद लाभ आम आदमी तक पहुंचने में समय लगेगा। अब यह देखना होगा कि कौन इस लाभ को आम आदमी तक पहुंचने नहीं दे रहा। इस बात पर भी गौर करना होगा कि देश में विकास के नाम पर कोई ऐसी तिकड़ी तो पैदा नहीं हो गई, जिसमें पूंजीपति, नौकरशाह और राजनीति के चुनिंदा लोगों का गठजोड़ बन गया हो। क्या यही गठजोड़ तो नहीं जो लोक कल्याण के रास्ते में दीवार बन रहा है ?
Date: 21-07-25
विकट और विकराल समस्या
विनीत नारायण
पिछले दिनों खबर छपी कि उत्तर प्रदेश में 2 हजार पदों के लिए 29 लाख आवेदन प्राप्त हुए। एक बार ऐसी भी खबर आई कि आईआईटी से पास हुए 38 फीसद युवाओं को रोजगार नहीं मिला। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कभी कोई सरकारी पद पर भर्ती खुलती है तो कुछ हजार पदों के लिए लाखों आवेदन आ जाते हैं। फिर वो पद छोटा हो या बड़ा, उस पद की योग्यता से अधिक योग्य आवेदक आवेदन देते हैं। बात बिहार की हो, उत्तर प्रदेश या देश में किसी अन्य राज्य की, जब भी एक पद पर उम्मीद से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो स्थिति अनियंत्रित हो जाती है। आज के दौर में अगर ‘मेनस्ट्रीम मीडिया’ किन्हीं कारणों से ऐसे सवालों को जनता तक नहीं पहुंचाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जनता तक वह सवाल पहुंच नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों इंटरव्यू देखे जा सकते हैं, जो बेरोजगारी की भयावह समस्या से जूझते युवाओं की हताशा दशति हैं। जब ये युवा रोजगार की मांग लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तो इन राज्यों की सरकारें पुलिस से इन पर डंडे बरसाती हैं। अगर युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की भी उम्मीद नहीं होगी तो हार कर उन्हें निजी क्षेत्र में जाना पड़ेगा और निजी क्षेत्र की मनमानी का सामना करना पड़ेगा।
दिक्कत यह है कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं बहुत तेजी से घटती जा रही हैं। इससे और हताशा फैल रही है। नौकरी नहीं मिलती तो युवाओं की शादी नहीं होती और उनकी उम्र ण बढ़ती जाती है। समाजशास्त्रीय शोधकर्ताओं को इस विषय पर शोध करना चाहिए कि करोड़ों बेरोजगार युवाओं की हताशा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देश के आर्थिक-सामाजिक ढांचे को देखते हुए शहरों में अनौपचारिक रोजगार की मात्रा को क्रमशः घटा कर औपचारिक रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। देश की सिकुड़ती अर्थव्यवस्था के कारण बेरोजगारी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। एक शोध के अनुसार भवन निर्माण क्षेत्र में 50%, व्यापार, होटल और अन्य सेवाओं में 47%, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में 39% और खनन क्षेत्र में 23% बेरोजगारी फैल चुकी है। चिंता की बात
यह है कि ये वो क्षेत्र हैं, जो देश को सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। इसलिए इन आंकड़ों का प्रभाव भयावह है। जिस तीव्र गति से ये क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं, उससे तो और भी तेजी से बेरोजगारी बढ़ने की स्थितियां पैदा हो रही हैं। दो वक्त की रोटी का भी जुगाड़ न कर पाने की हालत में लाखों मजदूर और अन्य लोग जिस तरह लॉकडाउन शुरू होते ही पैदल ही अपने गांवों की ओर चल पड़े थे, उससे इस स्थिति की भयावहता का पता चलता है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण एशिया के देशों में अनौपचारिक रोजगार के मामले में भारत सबसे ऊपर है, जिसका मतलब हुआ कि देश में करोड़ों मजदूर कम मजदूरी पर मुश्किल हालात में काम करने पर मजबूर हैं, जहां इन्हें अपने बुनियादी हक भी प्राप्त नहीं हैं। इन्हें नौकरी देने वाले जब चाहें रखें, जब चाहें निकाल दें क्योंकि इनका ट्रेड यूनियनों में भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार भारत में 53.5 करोड़ मजदूरों में से 39.8 करोड़ दयनीय अवस्था में काम करते हैं, जिनकी दैनिक आमदनी 200 रुपये से भी कम होती है। इसलिए मोदी सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली; शहरों में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं क्योंकि पिछले 7 वर्षों में बेरोजगारी का फीसद लगातार बढ़ता गया है। दूसरा, शहरी मजदूरों की आमदनी कैसे बढ़ाएं जिससे उन्हें अमानवीय स्थिति से बाहर निकाला जा सके। इसके लिए तीन काम करने होंगे। भारत में शहरीकरण का विस्तार देखते हुए शहरी रोजगार बढ़ाने के लिए स्थानीय सरकारों के साथ समन्वय करके नीतियां बनानी होंगी। इससे यह लाभ भी होगा कि शहरीकरण से जो बेतरतीब विकास और गंदी बस्तियों का सृजन होता है,उसको रोका जा सकेगा। इसके लिए स्थानीय शासन को अधिक संसाधन देने होंगे। दूसरा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन वाली विकासात्मक नीतियां लागू करनी होंगी। तीसरा; शहरी मूलभूत ढांचे पर ध्यान देना होगा जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी सुधरे। चौथा; देखा यह गया है कि विकास के लिए आवंटित धन का लाभ शहरी मजदूरों तक कभी नहीं पहुंच पाता और ऊपर के लोगों में अटक कर रह जाता है। इसलिए नगर पालिकाओं में विकास के नाम पर खरीदी जा रही भारी मशीनों की जगह मानव श्रम आधारित शहरीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा तो शहरों में रोजगार बढ़ेगा। पांचवां शहरी रोजगार योजनाओं को स्वास्थ्य और सफाई जैसे क्षेत्र में तेजी से विकास करके बढ़ाया जा सकता है क्योंकि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की यह हालत नहीं है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार दे सके। होती तो वे गांव छोड़ कर शहर नहीं गए होते।
मौजूदा हालात में यह सोचना कि पढ़े-लिखे युवाओं के लिए ऐसी योजना लानी पड़ेगी जिससे इनको भी रोजगार मिल जाए पर ऐसा करने से करोड़ों बेरोजगारों का छोटा सा अंश ही संभल पाएगा जबकि बेरोजगारों में ज्यादा तादाद उन नौजवानों की है, जो आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी बेरोजगार हैं। उनका आक्रोश बढ़ चुका है, और सरकारी तंत्र द्वारा नौकरी की बजाय लाठियों ने आग में घी का काम किया है।
कुछ वर्ष पहले सोशल मीडिया पर एक व्यापक अभियान चला कर बेरोजगार नौजवानों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन को ही ‘बेरोजगारी दिवस’ के रूप में मनाया था। उस समय इसी कॉलम में मैंने कहा था कि यह एक खतरनाक शुरुआत है जिसे केवल वादों से नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में शिक्षित रोजगार उपलब्ध करा कर ही रोका जा सकता है। मोदी ने 2014 के अपने चुनाव अभियान के दौरान प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार सृजन का अपना वादा निभाया होता तो आज ये हालात पैदा न होते। यहां यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि कोई भी राजनैतिक दल, जो अपने चुनाव अभियान में बेरोजगारी दूर करने का सपना दिखता है, सत्ता में आने के बाद अपना वादा पूरा नहीं करता । इसलिए सभी राजनैतिक दलों को मिल बैठ कर इस भयावह समस्या के निदान के लिए एक नई आर्थिक नीति पर सहमत होना पड़ेगा जिसके माध्यम से देश की संपदा चंद हाथों में सीमित होने की बजाय उसका विवेकपूर्ण बंटवारा हो ।
Date: 21-07-25
समझौते की सही शर्त पर अड़े भारत
आलोक जोशी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
ऐसा लगने लगा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्दी हो सकता है। इसकी रूपरेखा क्या होगी और यह कैसे होगा, यह रहस्य अब भी बरकरार है। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडोनेशिया की तर्ज पर भारत से व्यापार समझौता हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के बाजार उनके लिए पूरी तरह खुल जाएंगे।
इन बातों का क्या अर्थ है, यह तो तभी पता चलेगा, जब समझौता सामने होगा, मगर इंडोनेशिया को देखें, तो वहां अमेरिका से जाने वाले माल पर कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा, जबकि इंडोनेशिया से अमेरिका को निर्यात होने वाले माल पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि इंडोनेशिया अमेरिका से 15 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पाद, यानी तेल गैस खरीदने को भी राजी हुआ है और 4.5 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद भी खरीदेगा। यही नहीं, वह बोइंग के 50 विमान भी खरीदेगा |
अब अगर मान लें कि ट्रंप भारत के साथ भी ऐसा ही समझौता करने की सोच रहे हैं, तो क्या भारत अमेरिका को ऐसा ही खुला मैदान सौंप देगा ? हालांकि, यहां याद रखना चाहिए कि ट्रंप ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेकर कहा था कि भारत में अमेरिकी उत्पादों पर 52 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है और जवाब में वह भारतीय उत्पादों पर सिर्फ 26 प्रतिशत शुल्क लगा रहे हैं। इसके पहले वह एलान कर चुके थे कि सभी देशों पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क तो लगेगा ही और उसके ऊपर जवाबी शुल्क लगाया जाएगा, जिसकी दर सबके लिए अलग-अलग बताई गई। यानी, भारत पर कुल 26 प्रतिशत शुल्क लगना था। हालांकि, कुछ ही समय बाद उन्होंने रेसिप्रोकल, यानी जवाबी टैरिफ टालने का एलान किया और तब से वह एक के बाद दूसरे देश के साथ समझौते कर रहे हैं या फिर उनको चिट्टियां भेजकर टैरिफ का एलान कर रहे हैं। बहुत से कूटनीतिज्ञ मानते हैं कि ऊंची दरों पर टैरिफ का एलान कर ट्रंप मोलभाव के लिए दबाव बना रहे हैं। जैसे-जैसे समझौते हो रहे हैं, वैसे-वैसे इस बात में दम भी दिख रहा है।
बहरहाल, एक बात तो तय है कि समझौता जिन भी शर्तों पर होगा, भारत के लिए, खासकर व्यापार और उद्योग जगत के लिए यह अच्छी खबर होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर ट्रंप और टैरिफ एक पतले धागे से टंगी तलवार की तरह लटक रहे हैं। इस चक्कर में भविष्य का खाका खींचना या कोई योजना बनाना लगभग असंभव हो गया है। कहा जाता है, अच्छी खबर आने में भले ही देर हो, बुरी खबर जितनी जल्दी मिल जाए, इंसान उतनी अच्छी तैयारी कर सकता है। इसीलिए अब भारत में भी लोग समझौते की शर्तों से ज्यादा इस डील के होने का इंतजार कर रहे हैं।
यहां एक खास बात यह है कि अब ट्रंप प्रशासन भी इस मसले को जल्दी निपटाने के मूड में है। एक तो वह ‘भारत जैसा बड़ा बाजार हाथ से जाने नहीं दे सकता।
दूसरा, अब अमेरिका में टैरिफ का असर दिखने लगा है, यानी वहां महंगाई भड़क रही है। ऐसे में, अगर जल्द समझौते नहीं हुए, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मंदी का संकट बढ़ सकता है। दूसरी तरफ, ताजा आंकड़े दिखा रहे हैं कि जून के महीने में भारत द्वारा अमेरिकी निर्यात में 23 प्रतिशत का उछाल आया है, जबकि अमेरिका से आयात में 10 फीसदी की गिरावट आई है। यह आंकड़ा देखकर भ्रम हो सकता है। कुछ लोग दावा भी करने लगे हैं कि अब यह सिलसिला तेज होगा और भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार बनने की तरफ बढ़ रहा है। मगर ध्यान रहे, यह अपवाद है।
दरअसल, ऊंचे सीमा शुल्क की आशंका में वहां के ज्यादातर बड़े व्यापारियों ने विदेश से भारी मात्रा में माल आयात करके ‘स्टॉक’ कर लिया है, ताकि काफी समय तक ये नए टैरिफ से बचे रह सकें। इसके बावजूद अमेरिका में खुदरा महंगाई की दर 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह फरवरी के बाद से महंगाई दर का सबसे ऊंचा स्तर है। ऐसे में, आसानी से समझा जा सकता है कि टैरिफ वृद्धि का पूरा असर आने के बाद क्या होगा !
इसलिए यह समझना जरूरी है कि भारत इस वक्त टैरिफ के बोझ से दबने की आशंका से नहीं जूझ रहा है, पर यह खुशफहमी भी ठीक नहीं है कि अमेरिका दबाव में आने वाला है। शायद दोनों ही तरफ से जो टीमें बातचीत में जुटी हैं, उनको यह बात समझ में आ रही है, इसीलिए बातचीत अटकती हुई दिखती भले हो, मगर लगातार चलती रही है।
टैरिफ की चर्चा शुरू होने के साथ ही बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने हिसाब लगाया था कि अगर अमेरिका ने भारत से आयात पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, तो उससे लगभग 14.6 अरब डॉलर की ड्यूटी लग जाएगी। इसका सबसे बड़ा असर भारत से अमेरिका जाने वाले ऑटो पार्ट्स और बायोफार्मा उत्पादों के दाम पर पड़ेगा। हालांकि, कीमत अमेरिकी उपभोक्ता को ही चुकानी होगी, लेकिन इसका असर भारतीय कंपनियों के कारोबार पर दिख सकता है। उसका यह भी कहना था कि इसके बावजूद भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जीडीपी सालाना 6.4 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ता रहेगा और अगले दशक तक भारत विश्व व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।
मगर अमेरिका को छोड़कर भी दुनिया नहीं चल सकती, इसलिए अभी उसके साथ टैरिफ समझौता होना भारत के लिए भी जरूरी है। भारत अपने उन उद्योगों के लिए अमेरिका का बाजार खुले रखना चाहता है, जिनमें सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो दूसरी तरफ, अमेरिका हथियारों व औद्योगिक उत्पादों के अलावा अपने कृषि उत्पादों और मांस, मछली, अंडे व दूध जैसी चीजों के लिए भी यहां बड़ा बाजार देख रहा है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत जीएम फसलों के लिए रास्ता नहीं खोलना चाहता और डेयरी उत्पादों के लिए भी। दूध के मामले में तो देश के भीतर शाकाहार और मांसाहार की बहस भी खड़ी हो गई है।
बहरहाल, बातचीत का अंदाज बता रहा है कि रास्ता बहुत दूर नहीं है। मगर भारत को यह ख्याल रखना होगा कि इंडोनेशिया जैसा समझौता हमारे लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं हो सकता। भारत जहां भी अमेरिका को रियायत देगा, बदले में उसे भी वैसा ही फायदा मिलना जरूरी है। उम्मीद है, ऐसा ही होगा।