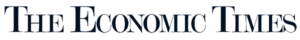21-07-2016 (Important News Clippings)
To Download Click here.
Date: 21-07-16
संकीर्णता के लिए सबक है गुजरात का दलित आंदोलन
Date: 20-07-16
स्वागत योग्य फैसला
उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्रि केट को राजनैतिक रसूख और पैसा बनाने की मशीन के रूप में इस्तेमाल करने वालों पर कुछ अंकुश लगेगा। अदालत ने न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की सिफारिशों को कुछ मामूली संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है और उन्हें बीसीसीआई में लागू करने का फैसला सुना दिया है। इससे क्रि केट को अपने रसूख और रुतबा बढ़ाने का साधन बनाने वाले नेताओं और कारोबारी शख्सियतों को बाहर का रास्ता तो नहीं दिखाया जा सकेगा, लेकिन उन पर थोड़ा अंकुश जरूर लग जाएगा। फैसले के सबसे महत्त्वपूर्ण दो प्रावधान हैं, जिनका बीसीसीआई विरोध करता आया है। एक, क्रि केट संघों में नेताओं के काबिज होने की उम्र सीमा 70 वर्ष कर दी गई है। इससे शरद पवार और श्रीनिवासन जैसे लोग इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। दूसरे, हर राज्य को एक वोट का अधिकार होगा। इससे महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों पर अंकुश लग जाएगा, जहां तीन-तीन संघ काबिज हैं और जिनको सियासी नेता अपनी ताकत दिखाने का साधन बनाते हैं। बीसीसीआई की दलील यह थी कि इससे पूर्वोत्तर जैसे उन राज्यों को भी बेमतलब वोटिंग अधिकार हासिल हो जाएंगे, जिनका क्रि केट से खास नाता नहीं है और ये राजनैतिक उठा-पटक का साधन बन जाएंगे। अदालत ने बीसीसीआई की इस दलील को ठुकरा दिया। जिन राज्यों में एक से अधिक संघ हैं, उन्हें बेमानी तो नहीं बनाया गया, लेकिन उन्हें बारी-बारी से वोटिंग का अधिकार दिया गया है। यानी एक साल इनमें कोई एक संघ को ही उस राज्य से वोट का अधिकार होगा। दरअसल, बीसीसीआई देश के ताकतवर सियासी और समृद्ध शख्सियतों के ऐसे क्लब में बदल गया है, जिनका क्रि केट के खेल से शायद ही कोई रिश्ता है। यों तो देश में हर खेल संगठन राजनैतिक नेताओं के लिए अपना रुतबा जताने के साधन हैं मगर क्रि केट की हैसियत हमारे देश में खासकर पिछले कुछ दशकों से ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है, जिससे हासिल होने वाले रुतबे और कमाई का कोई जोड़ नहीं है। इसमें सट्टेबाजी और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के भी बीज पड़ गए हैं, बल्कि उन पर अंकुश लगाने की कोशिशों का भी तरह-तरह की दलीलों के बहाने विरोध होता आया है। पिछली यूपीए सरकार के दौरान खेल संघों की सफाई के लिए लाया जाने वाला विधेयक इसी विरोध के चलते बेमौत मर गया। शायद सर्वोच्च अदालत की पहल से कुछ सफाई हो पाए।
Date: 21-07-16
टकराव पर आमादा चीन
दक्षिण चीन सागर में द्वीपों की संख्या 250 है। यहां किसी भी द्वीप पर इंसान नहीं रहते हैं। कई तो पानी के अंदर स्थित हैं। इनको तीन द्वीप समूहों में बांटा गया है। पहला, स्पार्टली द्वीपों पर अधिकार को लेकर ब्रूनेई, चीन, मलेशिया, फिलीपींस, ताईवान और वियतनाम के बीच विवाद है। दूसरा, पार्सेल द्वीपों पर अधिकार को लेकर चीन, ताईवान और वियतनाम के बीच विवाद है। वर्तमान में इन पर चीन का कब्जा है। तीसरा, प्रतास द्वीपों पर चीन, ताईवान और फिलीपींस दावा जताते हैं, लेकिन अभी इन पर ताईवान का कब्जा है। इसके अतिरिक्त मैकलेसफील्ड बैंक पर चीन, ताईवान और फिलीपींस अपना दावा जताते हैं।
चीनी समुद्री विवाद दशकों पुराना है। पूर्वी चीन सागर में दियाओ या सेनकाकू की संप्रभुता को लेकर विवाद की जड़ें 1894 के चीन-जापान युद्ध से जुड़ी हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की पराजय और शीत युद्ध के बाद के भूराजनीतिक घटनाक्रमों के साथ ही द्वीपों पर अधिकार को भी लेकर समस्या खड़ी हो गई। दक्षिण चीन सागर में आर्थिक जोन पर मिलते-जुलते दावे का भी अपना एक इतिहास है। दावेदार देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित ग्लोबलाइजेशन और हालिया घटनाक्रमों ने इन विवादों को फिर से हवा दी है। चीन ने अपने आर्थिक उत्थान के साथ-साथ दोनों सागरों में सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ाया है। हालांकि इसी दौरान दूसरे देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई है और उनकी सैन्य क्षमताओं में भी इजाफा हुआ है। परिणाम स्वरूप उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है।
हाल के वर्षों में चीन ने दक्षिण चीन सागर में हजारों वर्ग फीट क्षेत्र पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उसने वहां कृत्रिम द्वीप और रनवे, भवन, सेटेलाइट कम्युनिकेशन एंटिना आदि का निर्माण किया है। उसकी हरकतों ने पड़ोसी देशों और अमेरिका को यह सवाल पूछने के लिए मजबूर किया है कि क्या उनका उपयोग सिर्फ असैन्य उद्देश्यों के लिए होगा, जैसा कि बीजिंग ने दावा किया है। चीन द्वारा कृत्रिम द्वीप निर्माण से इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर संकट खड़ा हुआ है। उसने अपने सभी द्वीपों को लड़ाकू विमान, मिसाइल और मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैस किया है। जाहिर है, इससे शक्ति संतुलन चीन के पक्ष में झुकने की संभावना है। इन विवादित द्वीपों पर सेना की उपस्थिति निश्चत रूप से चीन की मारक क्षमता को दक्षिण और पूर्व में करीब एक हजार किलोमीटर और बढ़ा देगी।
चीन पार्सेल और स्पार्टली द्वीप समूहों पर कृत्रिम द्वीप के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर कर रहा है। बीजिंग ने दिसंबर 2013 के बाद से 3000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर पुन: दावा पेश किया है। यह दूसरे सभी दावेदारों द्वारा पिछले चार सालों में किए गए दावे से अधिक है। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी उपग्रह की तस्वीर में स्पार्टली द्वीप में सुबी रीफ और फेयरी क्रॉस रीफ पर चीन द्वारा अप्रत्याशित गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसमें साफ नजर आ रहा है कि वह वहां हवाई पट्टी, बांध और राडार तथा निगरानी संरचना का निर्माण कर रहा है।
1947 में चीनी सरकार ने दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय दावों का सीमांकन किया था। उसने मैप पर 11 डैश के साथ यू-आकार की लाइन बनाई, जो कि दक्षिण चीन सागर के अधिकांश क्षेत्र को समाहित किए हुए था। 1953 में इस मैप से टोंकिंग की खाड़ी को हटा दिया गया। परिणामस्वरूप दो डैश कम हो गए और उसके बाद से दक्षिण चीन सागर विवाद को नाइन डैश लाइन के नाम से जाना जाता है। नाइन डैश लाइन के साथ चीन दक्षिण चीन सागर के नब्बे फीसद जल क्षेत्र पर अपना दावा जताता है। 1995 में चीन ने मिसचीफ रीफ पर कब्जा कर लिया था और वहां मछुआरों के लिए एक आश्रय का निर्माण किया, जिसका प्रयोग उसके नौसैनिक समुद्री परिवहन पर नजर रखने के लिए भी करते हैं। चूंकि मिसचीफ रीफ पर फिलीपींस अपना दावा जताता रहा है, लिहाजा मनीला ने तुरंत ही आसियान देशों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन चीन ने उसके विरोध को नकार दिया और उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। 2009 में चीन ने संयुक्त राष्ट्र को एक मैप सौंपा, जिसमें नाइन डैश लाइन के अंतर्गत आने वाले द्वीपों और जलक्षेत्र पर अपने दावे की बात कही थी। 2013 में फिलीपींस चीन के साथ इस विवाद को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले गया। न्यायालय ने 12 जुलाई को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चीन के दक्षिण चीन सागर पर किसी ऐतिहासिक अधिकार की पुष्टि नहीं होती। मध्यस्थता न्यायालय ने फिलीपींस की संप्रभुता के अधिकारों का हनन करने के लिए चीन की निंदा भी की। फैसले में कहा गया कि चीन ने कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर वहां के पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। जापान, वियतनाम और फिलीपींस ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन चीन ने इस फैसले को कागज का पुलिंदा बताते हुए नकार दिया। विवादित जलक्षेत्र पर एक और दावेदार ताईवान ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को नहीं माना। वियतनाम ने कहा कि फैसला विवाद के समाधान के लिए कूटनीति और कानूनी प्रक्रिया की ओर बढऩे के रास्ते खोलता है। जापान ने बीजिंग की सेना की सीनाजोरी को लेकर चिंता व्यक्त की। भारत ने सभी देशों से आग्रह किया कि ट्रिब्यूनल के फैसले का सम्मान करें।
इस फैसले के गहरे सामरिक निहितार्थ होंगे। यह दक्षिण चीन सागर में तनाव में इजाफा करेगा। चीन ने संकेत दिया है कि वह दक्षिण चीन सागर में एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा करने जा रहा है। इसे आसियान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका द्वारा चुनौती मिलने की संभावना है। भारत के लिए इसका प्रभाव सकारात्मक होगा। यह दक्षिण चीन सागर में भारत को कानूनी रूप से मुक्त आवागमन का अधिकार देता है। नई दिल्ली अब वियतनाम से तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए किए गए वादे को पूरा कर सकती है। इससे भारत, अमेरिका, आसियान और जापान के बीच नौसैनिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। फैसले को अस्वीकार करने से चीन विश्व समुदाय में अलग-थलग पड़ सकता है।
[ लेखक ब्रिगेडियर ( रि.) आरपी सिंह हैं ]
Date: 21-07-16
संवैधानिक पद पर सवाल
केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों या इनसे जुड़े मुद्दों, विवादों पर चर्चा एवं उनके संभावित समाधान के लिए गठित शीर्ष संस्था इंटर स्टेट काउंसिल की 11वीं बैठक 16 जुलाई को दिल्ली में संपन्न हुई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस परिषद की यह बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह पूरे दस साल बाद आयोजित हुई है। बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें एक महत्वपूर्ण विषय था राज्यपाल के पद को लेकर, जिस पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सवाल खड़े किए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो सीधे-सीधे यह मांग कर दी कि राज्यपाल का पद ही समाप्त कर दिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान है। फिर इस संविधानिक पद को खत्म करने की मांग क्यों की जा रही है? इसी से जुड़ा प्रश्न है कि राज्यपाल का पद विवादों में क्यों रहता है? फिर, क्या यह मांग राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है? और इस विवाद के हल की क्या संभावित दिशा हो सकती है?
दरअसल विवाद की जड़ में राज्यपाल की नियुक्ति का ढंग, उसकी अर्हता, पदावधि, उसकी विवेकाधीन शक्ति और उसके कार्य करने के तरीके आदि प्रमुख हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। व्यवहार में यह नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर होती है। इस अर्थ में राज्यपाल एक तरह से केंद्र सरकार का प्रियपात्र व्यक्ति होता है। इसी अनुच्छेद में विवाद के बीज छिपे हुए हैं, जिनको खाद-पानी देने का काम अन्य संवैधानिक प्रावधान करते हैं। स्वाधीनता के कुछ ही वर्षों के बाद से देखा जाने लगा कि यह पद केंद्र में सत्तासीन पार्टी के राजनेताओं का अड्डा अथवा आरामगाह बन गया। इसी तरह अनुच्छेद 156 के अनुसार आमतौर पर राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्षों के लिए होगा, लेकिन वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जब चाहे उसे हटा सकती है। इस रूप में केंद्र सरकार उस पर मनचाहा दवाब बनाए रहती है।
संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि किन आधारों पर राज्यपाल को हटाया जा सकता है। सिर्फ राजनीतिक पसंद-नापसंद की वजहों से यह खेल होता रहा है, जिसकी शुरुआत लंबे समय तक केंद्र में आसीन कांग्रेस सरकार द्वारा हुई थी। उसी क्रम में 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने पूर्व की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त अनेक राज्यपालों का त्यागपत्र मांग लिया था। 1991 में जब नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार बनी तो यही प्रक्रिया दोहराई गई और वीपी सिंह एवं चंद्रशेखर सरकार के समय में नियुक्त दर्जन भर राज्यपालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2014 में आई वर्तमान राजग सरकार ने भी कमोबेश यही रुख अपनाया। हालांकि 2010 में बीपी सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि राज्यपालों को मनमाने ढंग से केंद्र सरकार नहीं हटा सकती। अगर बर्खास्तगी दुर्भावनापूर्ण या स्वेच्छाचारी है तो पीडि़त व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है तथापि इस निर्णय के बावजूद भी केंद्र सरकार येन-केन प्रकारेण राज्यपालों को हटा सकने में सक्षम है।
राज्यपाल की अर्हता भी समस्या से परे नहीं है। राज्यपाल के लिए दो अर्हताएं हैं। भारत का नागरिक होना और 35 वर्ष का होना। हालांकि इसमें एक अन्य परंपरा भी जुड़ गई है कि उसे उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे। हालांकि कुछ मामलों में इस परंपरा का उल्लंघन भी हुआ है। विवाद राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर भी है। अक्सर आरोप लगाया जाता है कि वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करने के बजाय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में ही ज्यादा कार्य करता है। चाहे किसी विधेयक को मंजूरी देने मुद्दा हो (गुजरात के राज्यपाल के रूप में कमला बेनीवाल की भूमिका विवादास्पद रही थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नौ बिलों को मंजूरी देने में अड़ंगा लगाया) अथवा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का मसला हो (2005 में झारखंड के राज्यपाल द्वारा अनुचित रूप से शिबू सोरेन की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति) अथवा राष्ट्रपति शासन की अनुचित अनुशंसा का मामला हो (उत्तराखंड का हालिया प्रकरण) या फिर अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल की विवादास्पद भूमिका की हालिया घटना हो-राज्यपालों के कामकाज अक्सर विवादित रहे हैं।
इन्हीं कारणों से गाहे-बगाहे इस पद को खत्म करने की मांग उठती रही है। लेकिन क्या यह मांग जायज है? खास तौर से विशिष्ट समस्याओं और विविधताओं से भरे भारत में हमारे अनेक राज्य जहां सीमावर्ती हैं तो दूसरी ओर अनेक राज्यों में ऐसी स्थानीय पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय हितों को ज्यादा तरजीह नहीं देतीं। इन स्थितियों में राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए अनिवार्यता भी। फिर समाधान क्या है? सही हल तो यही होगा कि राज्यपाल के पद को खत्म करने के बजाय उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया, अर्हता, पदावधि और विवेकाधीन शक्तियों को फिर से परिभाषित किया जाए। इस संदर्भ में सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, वाजपेयी सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग रिपोर्ट तथा पुंछी कमीशन रिपोर्ट हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। एक तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति गठित हो जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति हों। साथ ही पैनल बनाते समय मुख्यमंत्री की राय अवश्य ली जाए। दूसरे, उसका कार्यकाल पांच वर्षों के लिए सुनिश्चित हो। उसे पद से हटाना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए। तीसरे, कुछ नकारात्मक अर्हताएं भी तय हों, जैसे नौकरशाहों अथवा जजों के लिए अवकाश के बाद दो वर्ष की पाबंदी हो और विवेकाधीन अधिकारों का स्पष्ट रूप से कोडीफिकेशन हो ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके। देशहित सर्वोपरि है और उसके लिए राज्यपाल आवश्यक हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति पर तो पुनर्विचार करना ही होगा।
[ विभिन्न अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक रहे लेखक डॉ. निरंजन कुमार, सम्प्रति दिल्ली विवि में प्रोफेसर हैं ]
Date: 21-07-16
State-Owned Banks Ask For Lots More
The government’s capital infusion of .₹ 22,915 crore in 13 public sector banks (PSBs) provides immediate succour, but is insufficient to clean up their books and enable them to lend more to support growth. The more banks lend, the more capital they need to stay secure. That’s a huge challenge, with gross nonperforming assets at 11.5% of total lending at end-March. Basel III norms mandate banks to have capital of at least 9% of their risk-weighted assets and a capital buffer of equity of 2.5% of their assets. ICRA estimates PSBs Tier 1 capital requirement at .₹ 1.7-2.1 trillion over FY 2017-2019. All of it cannot come from the government. A majority state-owned holding company, whose equity is the pooled government equity in PSBs, could leverage that manifold to raise resources to hold 51% stakes in all PSBs. A Banks Board Bureau is functional. It can appoint the boards of PSBs and hold them to account. Investors also would get an opportunity to buy shares in some of the most profitable state-owned banks. That would be one way of increasing PSBs’ capital base without losing majority state ownership. But if the government is willing to abandon the theology of majority state ownership of PSBs, the banks could raise lots of fresh capital. Control is exercised in private entities, including banks, by those who hold chunks of equity that fall well short of 50%. With ownership of over 26%, the government would still be powerful enough a shareholder to run the board, if it wants to retain control of some key banks.
In 2014, the RBI allowed bonds, raised as part of the bank’s core capital, to be converted into equity. Bail-in-bonds that can be converted into equity, if a bank’s capital falls below a set trigger level, are another way to raise loss absorbing capacity.
Date: 21-07-16
From Independence to Freedom
Yes, that’s the socialist dream
It is likely that future Indian schoolchildren will be made to learn two important dates from the 20th century: 1947 and 1991. The importance of 1947 is obvious, but why is 1991 a turning point of similar importance?
One could argue that 1947 saw political power shift from a foreignborn elite to an Indian-born elite. This was undoubtedly an important change, but it carried forward a top-down mindset that a tiny group of ‘wise men’ knew what was best for the rest of the population. This thinking was embodied in every level of national life — economic, social and cultural.
Thus, a tiny group of planners led by PC Mahalanobis could decide how to allocate all economic resources. A handful of business conglomerates cornered all industrial licences. Encouraged by the thinking of Le Corbusier, urban planners could encode rigid masterplans that decided how people led their lives into perpetuity. A small clique of intellectuals and editors, supported by state-controlled media and academia, could tell people what to think.
For all the socialist rhetoric, this system perpetuated the power of a small elite — political dynasties, business dynasties, even entertainment dynasties flourished. It should be no surprise that, with the ex- ception of the Ambanis, the top business families of the 1990s were the same as those of the 1940s.
Defenders of the Nehruvian project will argue that the failures of the system were not apparent for decades. Far from it. The term ‘License Raj’ was coined in the 1950s by C Rajagopalachari, who predicted the corruption and inefficiency that was to follow. LIC was nationalised in 1956 and within months its resources were being plundered by politically linked groups. This resulted in the Mundhra Scandal of 1958 that was exposed by Feroze Gandhi. Rather than acknowledge the problem, Jawaharlal Nehru cut off links with his son-in-law.
It was more than obvious by the 1970s that the Nehruvian model had failed. However, establishment economist Raj Krishna dubbed the poor economic performance as the ‘Hindu rate of growth’. In other words, India’s cultural and religious traditions were at fault and not economic policies. India had failed Nehru and not the other way around. Enormous resources were used to bolster intellectual justification for the failing system. Institutions like JNU were created explicitly for this purpose and an elaborate system of national awards and positions was built to promote loyalists as public expense.
Thus, when reforms finally came in 1991, it was due to economic collapse and not a change in mindset. With a few notable exceptions, the leading Indian intellectuals of that time were unanimous that liberalisation was a bad thing.
So, when finance minister Manmohan Singh presented the Budget in February 1992, he felt it was necessary to say, “Our nation will remain eternally grateful to Jawaharlal Nehru for his vision….” He concluded the speech with “Tonight I feel like I am going to the theatre. Let the assassins be informed, I am prepared for the onslaught.”
Only when one re-reads these words that one recognises the political risks Prime Minister Narasimha Rao was taking by liberalising the economy. He was not just unwinding industrial licensing but a quasi-feudal oligarchy that pervaded every sphere of life in India — a process that is still not complete.
It is now 25 years since the liberalisation process was initiated. New business leaders, writers, sports stars, and more broadly a new middle class has emerged who are not beholden to public sector largesse. What is extraordinary is that despite obvious improvement in economic and social indicators, reformers still struggle to make a case for basic changes.
The reason for this is that the intellectual and institutional framework of the Nehruvian project was not systematically replaced. It was only in 2014 that the Planning Commission was finally abolished. Academia remains in the firm grip of the old mindset.
Although remnants of the Nehruvian apparatus need to be unwound, the next 25 years should focus on building a new system. The alternative to the top-down, allpervasive Nehruvian State is not necessarily a minimalist, libertarian one. India needs a strong but limited State that focuses on creating an open framework that allows bottom-up innovation, risk-taking and social mobility.
The creation of such a State still needs political leadership, but one that addresses framework issues: basic infrastructure, internal/ external security, simple tax system and so on. Most importantly, the State must be able to enforce laws and contracts.
A bottom-up economic and social structure is all about how various entities interact independently with each other. Such a system cannot function with 34 million cases stuck in courts. This is why the next generation of reforms must be about transparent laws, quick judicial process and reliable policing.
Just as 1947 gave us independence from colonial rule, 1991 started the process that gave Indians freedom from a self-defeating mindset. The next big turning point in Indian history will be the year when we finally get serious about reforming the legal system. I hope 2017 will be that year.
Date: 21-07-16
End atrocities:
Government must act decisively against cow vigilantes who compound social divisions and economic losses
As Dalit protests escalate in Rajkot, Junagadh, Jamnagar, Rajkot and Amreli districts, the Gujarat government seems caught unawares. Many Dalits have attempted suicide, suggesting they are being pushed to the edge. Protests started after a Dalit, Balu Sarvaiya, and his family members were brutally assaulted and publicly flogged by a cow protection group for allegedly skinning a cow in Una town of Gir Somnath district. Though 16 people have been held in the case so far, the filming of the heinous act and dissemination of the video not only indicates the culture of sheer impunity that prevails on the ground but also suggests an act of Talibanist terror.
Bans on cow slaughter already existed on the statute books of many states. By tacking on to them draconian laws that invade people’s kitchens and criminalise even the consumption of beef, BJP state governments have contributed to the atmosphere of hysterical cow vigilantism which wasn’t a problem before the advent of NDA but seems to have enmeshed the country now.
Skinning dead bovine animals is the only source of income and livelihood for many Dalit families like Sarvaiya’s, providing an important input for the leather industry. This is a labour-intensive industry with an annual turnover of Rs 80,000 crore; India is the second largest producer of leather footwear and garments in the world and the Make in India initiative aims to more than double its turnover by 2020, providing employment to nearly 60 lakh people. Unleashing cow vigilantism thus undermines national economic goals such as creating jobs for India’s youth. This can’t be good news when India’s current growth is largely jobless.
By encouraging beating up on Dalits and minorities cow vigilantism has political repercussions too, including for BJP. It deepens the impression created after Rohith Vemula’s suicide that BJP is against Dalits. By creating insecurity among minorities it is a factor that feeds into the Kashmir riots. It’s worth remembering that tension has been building in the Valley since the murder of a truck driver in Udhampur over cow slaughter rumours late last year. Political and social polarisation are not in BJP’s, let alone the nation’s interest. It’s time now to take the strictest possible action against cow vigilantes and brutal moral policemen, but that alone won’t be enough. State governments must also send an unmistakable political signal by dialling back on draconian beef bans which are feeding the hysteria.
Date: 21-07-16
Securing the code
The endeavour for a common civil law must be to end discrimination, and not stamp majority might
Written by UPENDRA BAXI
Public and political debates surround the “paramount” duty under Article 44 that asks the state to endeavour to secure a Uniform Civil Code (UCC). These debates have particular poignancy for communities whose personal law is to be made “uniform” and for the political parties who promise to pilot a code. It is too emotional and volatile an issue to readily permit rational consensus. Proponents for change insist that almost seven-decades is too long a period for the state to not endeavour towards a UCC. In contrast are the claims that the time is not ripe and an establishment-centred hegemony should be avoided. A major twist has now been added to the tale by the demands of the movements for human rights of children as well as by the demands placed by women’s rights movements for laws and policies that do not discriminate on the basis of gender.
However, the constitutional promise itself is infinitely complicated. Public and political debates have not considered what exactly are the “duties” created by Article 44. So far, all interpretive efforts have eluded narrative coherence. The duty is not to merely to legislate but to “secure” a code. How long shall the state endeavour? Perhaps, the time has come for an amendment of this article and prescribing a time-bound schedule.
Has the state at all endeavoured? While there are many different standpoints, Law Commission Chair, Justice B.S. Chauhan, was right in saying that the elements of a UCC already exist in “some legislations where a common law was applicable to all without consideration of religion”, and that “most people are perhaps unaware that common code exists in many laws”. But his preliminary articulation suggesting the need to de-link the UCC from religion will surely be contested.
Perhaps by “uniform” we understand that all citizens should be subject to the same law, regardless of community, religion, and identity. But when the personal law stands anchored in the freedom to practice religion, state intervention may violate a fundamental right. Further, who decides what religion requires: The custodians or all the coreligionists? What legal and social meaning is to be invested in Article 51-A(f), which talks of the fundamental duty of all citizens “to value and preserve the rich heritage of composite culture”? When may this conflict with Article 51-A(e) that talks of the need to “renounce practices derogatory of women”? The duty (in clause “h”) to “develop the scientific temper, humanism and the spirit of enquiry and reform” reinforces social inclusion in religion and the state. How best to have legal controls over religious practices that hurt human rights warrants serious consideration from all sides.
And indeed when is a “code” a “code”? If codification is to avoid merely articulating majoritarian might, it ought to be a historically-calibrated state venture at social consensus. Here, adjudicatory leadership matters as much as national leadership. Is piecemeal normative cleansing of disvalued difference less eligible than a total UCC? Is reasoned judicial enunciation to be preferred over “state endeavour”? The question is: How best to secure a codification that genuinely endeavours to remove discrimination and prejudice against women’s and child rights?
The German historical jurist Fredrick von Savigny said (in mid-19th century) that codification involved both a “technical element” (the knowledge of customs that are to be codified) and a “political element” (the question of political will to codify). Do we know enough about the personal law of various tribal communities from which the UCC may choose? Or, the laws of various Hindu and Muslim communities? Do we know enough about the religious personal law of other Indian communities? It is a sad mistake to think that a UCC is all about Hindu-Muslim relations and identities.
The political element in India today must refer equally to political and judicial will. True, the Supreme Court has quite often subjected customary and codified personal laws to the equality and gender justice discipline of the Constitution and also said that a UCC is a desirable constitutional mandate which the state ought to follow more expeditiously. The court (Chief Justice T. S. Thakur, Justices A.K. Sikri, and R. Banumathi) has also said that it is the solemn duty of Parliament to enact a UCC. However, in response to a PIL filed in the Supreme Court, a bench of Justices Anil R. Dave and Adarsh Kumar Goel also directed the National Legal Services Authority of
India to re-examine the issue of “gender discrimination” suffered by Muslim women in the country.
The nascent Bharatiya Muslim Mahila Andolan, a national coalition of Muslim women with over 70,000 members across 13 states, recently collected around 50,000 signatures of Muslim women demanding the abolition of the triple talaq system of divorce. And it has sent a letter to Prime Minister Narendra Modi asking for reforms. Obviously, the authority is bound to take into account this petition. Besides, the Law Commission of India has been asked in June to submit a report on UCC.
It thus seems that there is a new political determination about UCC in the air. The difficult decisions ahead relate to the linkage between personal law system and religious and communitarian identity. While the UCC opponents maintain that the state may reform a community law only with their consent, it is also a moral principle that the consent should not be withheld unreasonably and permanently. The additional requirement that the state provides security and safety to every citizens is valid: A democratic state should neither become an “institutionalised riot system” (in Paul Brass’s words) nor should governance become a specialised sphere of managing “riot after riot” (to use the title of M.J. Akbar’s book).
Farrah Ahmed concludes that the existing personal law system “harms religious autonomy” (considered as self-respect) of those subject to it. However, she suggests a religious alternative dispute resolution (ADR), under which persons will devise their norms and choose religious arbitration or mediation, restrained only by legal protections against oppression. One hopes that ADR will find some resonance in state and civil society, as a prelude to a future UCC.
Date: 21-07-16
The coming revolution in Indian banking
Increasing penetration of smartphones, Aadhaar-linked bank accounts and a host of powerful open and programmable capabilities is set to create the ‘WhatsApp moment’ for Indian banking
Written by Nandan Nilekani
Once in a while a major disruption or discontinuity happens which has huge consequences. In 2007, the internet and the mobile phone came together in a whole new product called the smartphone. This phone, with its own operating system, such as the iOS or Android, could support over the top (OTT) applications. The messaging solution for the smartphone did not come from the giant telecom or internet companies. Instead, it came from WhatsApp, a start-up. WhatsApp does 30 billion messages a day, whereas all the telecom companies put together do 20 billion SMS messages per day. Such is the power of disruption!
Such a “WhatsApp moment” is now upon us in Indian banking. This discontinuity has been caused by several things coming together. Smartphones are growing dramatically and are expected to reach a penetration of 700 million by 2020. Over 1 billion Indian residents now have Aadhaar, an online biometric identity. The government promoting financial inclusion through the Jhan Dhan Yojana has led to over 200 million new bank accounts being opened. With the RBI giving licences to over 20 new banks, including small banks and payment banks, the competitive intensity of the sector is set to increase. One can visualise a future where every adult Indian has an Aadhaar number, a smartphone and a bank account. Already over 280 million Indian residents have an Aadhaar-linked bank account and around 1 billion direct benefit transfer (DBT) transactions have happened, whose value is in the billions of dollars.
On top of this, a set of powerful open and programmable capabilities, that are collectively referred to as the “India Stack” by the think-tank iSPIRT, has been created over the last seven years. Aadhaar provides online authentication using one’s fingerprint or iris, which can be done from anywhere. This can make transactions “presence less”. The e-KYC (know your customer) feature of Aadhaar enables a bank account to be opened instantly, just by using the Aadhaar number and one’s biometric. The e-sign feature enables online documents to be digitally signed with Aadhaar. The “digital locker” system enables the storage of such electronic documents safely and securely. All this can make the entire banking process “paperless”.
The final two layers of the “India Stack” have great relevance to the future of banking. The Unified Payment Interface (UPI) layer, a product built by the National Payment Corporation of India (NPCI), a non-profit company collectively owned by banks and set up in 2009, will revolutionise payments and accelerate the move towards a “cashless” economy. So “pushing” or “pulling” money from a smartphone will be as easy as sending or receiving an email. This product from NPCI is the latest in several payment systems that they have developed, from the National Financial Switch, National Automated Clearing House, and RuPay cards, to the Aadhaar Payment Bridge, the Aadhaar-enabled Payment System and IMPS, a real-time payment system.
The move to a “cashless” economy will be accelerated by the Aadhaar-enabled biometric smartphones. So credential checking in banking will move from “proprietary” approaches (debit card and PIN) to “open” approaches (mobile phone and Aadhaar authentication). As such, the holy grail of one-click two-factor authentication, now available only to giants like Apple, will be available to kids in a garage to develop innovative solutions.
Finally, as India goes from being a data-poor to a data-rich economy in the next two to three years, the electronic consent layer of the “India Stack” will enable consumers and businesses to harness the power of their own data to get fast, convenient and affordable credit. Such a use of digital footprints will bring millions of consumers and small businesses (who are in the informal sector) to join the formal economy to avail affordable and reliable credit.
As data becomes the new currency, financial institutions will be willing to forego transaction fees to get rich digital information on their customers. The elimination of these fees will further accelerate the move to a cashless economy as merchant payments will also become digital.
This will also shift the business models in banking from low-volume, high-value, high-cost, and high fees, to high-volume, low-value, low-cost, and no fees. This will lead to a dramatic upsurge in accessibility and affordability, and the market force of customer acquisition and the social purpose of mass inclusion will converge.
These gale winds of disruption and innovation brought upon by technology, regulations and government action, will fundamentally alter the banking industry. Payments, liabilities and assets will undergo a dramatic transformation as switching costs reduce and incumbents are threatened. As the insightful report from Credit-Suisse has so well explained, there is a $ 600 billion market capitalisation opportunity waiting to be created in the next 10 years. This will be shared between existing public and private banks, the new banks and new-age NBFCs. It may even go to non-banking platform players, which use the power of data to fine-tune credit risk and pricing, and make money from customer ownership and risk arbitrage.
The public sector banks, which occupy the commanding heights of the economy with a 70 per cent market share, will be particularly challenged. Even as they deal with the inheritance of their losses, they will have to cope with, and master, enormous digital disruption. This will require their owners, the government, to give them the autonomy and freedom to experiment and innovate.
To quote Shakespeare, “There is a tide in the affairs of men, which, taken at the flood, leads on to fortune”. The $ 600-billion opportunity is here. The WhatsApp revolution went unnoticed by incumbents. Normally such disruptive changes (like bubbles) are only recognised after they have happened. In this case, the forces of change are evident and can be anticipated. The opportunity for the banking sector has been called, and it is equally accessible to incumbents, both in the public and private sector, to the new banks, to the NBFCs and the tech companies. The future will belong to those who show speed, imagination and the boldness to embrace change.