
21-06-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
 Date: 21-06-25
Date: 21-06-25
Last word
HCs and trial courts must follow SC’s line on free speech
TOI Editorials
 The Constitution is clear – you have the right to freedom of speech and expression, subject to reasonable restrictions. But like an Ashokan edict carved in stone, the Constitution’s letter is only as good as the spirit of the institutions tasked with upholding it. In the Thug Life case, SC has once again struck a blow for free speech. While clearing the Kamal Haasan film’s release in Karnataka, it has made it abundantly clear that one person’s “hurt sentiments” are not a reasonable ground for curbing another’s right to expression: “In India…there will never be an end to the hurt sentiment phenomenon. But for that, right to free speech cannot be jeopardised…” Three months ago, in the Imran Pratapgarhi case, SC had forcefully made the same point: “Even if a large number of persons dislike the views expressed by another, the right of the person to express the views must be respected and protected.”
The Constitution is clear – you have the right to freedom of speech and expression, subject to reasonable restrictions. But like an Ashokan edict carved in stone, the Constitution’s letter is only as good as the spirit of the institutions tasked with upholding it. In the Thug Life case, SC has once again struck a blow for free speech. While clearing the Kamal Haasan film’s release in Karnataka, it has made it abundantly clear that one person’s “hurt sentiments” are not a reasonable ground for curbing another’s right to expression: “In India…there will never be an end to the hurt sentiment phenomenon. But for that, right to free speech cannot be jeopardised…” Three months ago, in the Imran Pratapgarhi case, SC had forcefully made the same point: “Even if a large number of persons dislike the views expressed by another, the right of the person to express the views must be respected and protected.”
As the chief arbiter of the land, SC could not have made itself clearer in March any more than it can now. There’s no way its word can be misunderstood or misinterpreted. Yet, Calcutta HC told a 22-year-old early this month: “Look, we have freedom of speech but that doesn’t mean you will go on to hurt others.” Then, Karnataka HC told Haasan: “You or any citizen have no right to hurt sentiments of the masses…” And lower courts’ views on free speech are generally even more stifling. This divergence of opinion within the judiciary has a chilling effect on free speech because there’s only one SC above hundreds of HCs and subordinate courts. If free speech is a pillar of democracy, and a tenet of the Constitution, it shouldn’t have to run the gauntlet with the hope of eventual salvation in the apex court.
Quantum challenge
Administrative reform is essential for India to make advances
Editorial
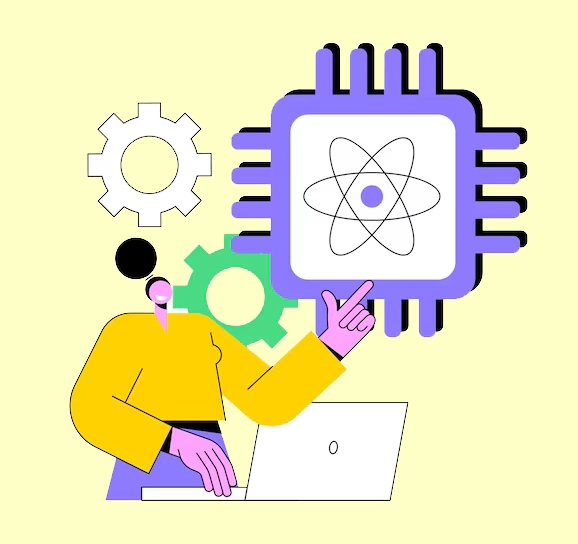 Scientists from IIT-Delhi and the DRDO recently demonstrated a key advance in quantum cybersecurity that stands to revolutionise how the world will communicate in the future. The world’s secrets are currently stored and communicated via channels that are protected by difficult mathematical problems. Over the years, an increasing amount of computing power available to certain actors has forced these problems to become difficult and nigh-uncrackable. The imminence of quantum computing requires this paradigm to change because quantum computers can (at least on paper) solve problems currently out of reach of the most powerful conventional supercomputers. Quantum cybersecurity is one prong of this change, promising to protect communication channels irrespective of the computing power available to malicious actors. The IIT-Delhi and DRDO team successfully demonstrated a quantum key-distribution scheme through one kilometre of free space on the institute’s campus. Such a technology allows two individuals (or stations) located a kilometre apart to securely access messages they send each other. If an eavesdropper tries to intercept any message, instantaneous changes in the keys the individuals use to decrypt the messages will reveal the channel has been compromised, and in a way that the eavesdropper cannot prevent. If scaled up to include satellites, the technology could allow stations anywhere in India to exchange information through a quantum network without fear of being compromised.
Scientists from IIT-Delhi and the DRDO recently demonstrated a key advance in quantum cybersecurity that stands to revolutionise how the world will communicate in the future. The world’s secrets are currently stored and communicated via channels that are protected by difficult mathematical problems. Over the years, an increasing amount of computing power available to certain actors has forced these problems to become difficult and nigh-uncrackable. The imminence of quantum computing requires this paradigm to change because quantum computers can (at least on paper) solve problems currently out of reach of the most powerful conventional supercomputers. Quantum cybersecurity is one prong of this change, promising to protect communication channels irrespective of the computing power available to malicious actors. The IIT-Delhi and DRDO team successfully demonstrated a quantum key-distribution scheme through one kilometre of free space on the institute’s campus. Such a technology allows two individuals (or stations) located a kilometre apart to securely access messages they send each other. If an eavesdropper tries to intercept any message, instantaneous changes in the keys the individuals use to decrypt the messages will reveal the channel has been compromised, and in a way that the eavesdropper cannot prevent. If scaled up to include satellites, the technology could allow stations anywhere in India to exchange information through a quantum network without fear of being compromised.
Herein lies the rub. Quantum communications is one of the four themes of the National Quantum Mission, approved in 2023 with an outlay of ₹6,003 crore until 2031. Many of the same problems assailing fundamental research in India have already beset research under the Mission, however. A small fraction of the outlay has been disbursed thus far even as venture capital flow into startups remains trivial. Scientists have complained that just-in-time funding, absence of single-window clearances, and documentation requirements have increased the duration of projects. There are persistent foreign hardware and software dependencies: materials required for specific use-cases, such as cryostats and sensors, need to be fabricated abroad while most quantum software stacks are currently implemented by multinational companies. Government pay does not match global offers and lack of timely access to resources has forced researchers to accept short-term contracts and rent equipment. In fact, India’s commitment, itself down from the ₹8,000 crore announced in 2020, is dwarfed by those of the U.S. and China, which are five- and 20-times higher, respectively. If the demonstration at IIT-Delhi is to scale, the government cannot simply ‘clip on’ scientific talent and technological and economic opportunity to existing infrastructure. Administrative reform is essential.
 Date: 21-06-25
Date: 21-06-25
सुनियोजित कदम से बनेगा उत्तम प्रदेश
संपादकीय
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) भारत के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। देश से वस्तुओं के कुल निर्यात में एमएसएमई खंड की हिस्सेदारी 45 फीसदी से अधिक है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इनका योगदान लगभग 30 फीसदी है। देश में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सेमीकंडक्टर जैसे मूल्यवान क्षेत्रों सहित बड़े औद्योगिक संकुलों को जिस तरह महत्त्व दिया जा रहा है उतना ही ध्यान एमएसएमई के विकास के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करने पर दिया जाना चाहिए। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सुनियोजित रूप से कदम बढ़ाता प्रतीत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की संख्या देश में सर्वाधिक है। राज्य में कुछ समय पहले विशेष रूप से एमएसएमई के लिए 11 जिलों में 15 औद्योगिक क्षेत्र तैयार करने से जुड़ी घोषणाएं हुई हैं। इनमें यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी शामिल है। राज्य में नए एमएसएमई के लिए 500 एकड़ जमीन का इंतजाम किया गया है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के ये प्रयास सही दिशा में हैं। एमएसएमई विभाग द्वारा तैयार मसौदा योजना के अनुसार इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 764.31 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 60 फीसदी है और राज्य के निर्यात में भी इसकी हिस्सेदारी 46 फीसदी तक पहुंच जाती है। राज्य की ऐसी इकाइयों की हिस्सेदारी देश के कुल एमएसएमई में लगभग 14 फीसदी है। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) जैसी विशेष योजनाएं परंपरागत एवं कारीगरी कौशल को नए सिरे से बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ओडीओपी योजना के माध्यम से परंपरागत एवं कारीगरी कौशल आधुनिक मूल्य श्रृंखला से जुड़ रहा है। राज्य ने भौगोलिक संकेतकों (जीआई) के मामले में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। देश में सर्वाधिक जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश स्थानीय उत्पादों के दम पर एक नया एवं विशिष्ट बाजार तैयार करने में सफल रहा है। वर्ष 2023-24 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 13 फीसदी रही जो प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) दर 7.5 फीसदी से आगे निकल गई। वर्तमान मूल्यों पर विनिर्माण राज्य की अर्थव्यवस्था में 27 फीसदी योगदान दे रहा है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के लगभग सभी जिलों में निवेश बढ़ रहा है। यह प्रगति एमएसएमई क्षेत्र को आगे बढ़ने में मदद करती है और एक संतुलित औद्योगिक तंत्र विकसित करने में भी सहायता मिली है।
ये सभी प्रयास उपयुक्त दशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं किंतु अब भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। महिला उद्यमिता की कमी सबसे अहम बिंदु है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य में मौजूद कुल एमएसएमई में महिलाओं द्वारा संचालित एमएसएमई की हिस्सेदारी मात्र 33 फीसदी है। यह अनुपात कई राज्यों की तुलना में कम है। लक्षित कौशल विकास, वित्त की उपलब्धता और महिला केंद्रित औद्योगिक संकुल रोजगार एवं उत्पादन और बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था चुनौती और अवसर दोनों पेश कर रही है। कृषि-प्रसंस्करण, खाद्य संरक्षण, ग्रामीण शिल्प और कृषि उपकरण विनिर्माण खंडों में अपार संभावनाएं हैं जिनका पर्याप्त लाभ नहीं उठाया गया है। इन खंडों में आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश मौजूद है। उदाहरण के लिए राज्य की खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति 2022-27 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य की 24,000 खाद्य-प्रसंस्करण इकाइयों में केवल 6 फीसदी ही ऐसी हैं जिनका सालाना राजस्व 20 करोड़ रुपये से अधिक है। यह स्थिति क्षमता एवं कारोबार विस्तार की संभावनाएं उपलब्ध होने का संकेत दे रही है। कृषि क्षेत्र को एमएसएमई से जोड़ने वाली मूल्य श्रृंखला मजबूत बनाने से किसानों की आय बढ़ सकती है और ग्रामीण क्षेत्र में संकट भी कम हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि एमएसएमई नीतियां केवल अवसंरचना एवं भूमि पर ही केंद्रित न रहें बल्कि नियम अनुपालन का बोझ घटाने, वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ढुलाई से जुड़ी बाधाएं भी दूर करने में योगदान दें। देश के सबसे बड़े राज्य में अधिक औद्योगिक उत्पादन एवं रोजगार के अवसर भारत की संपूर्ण आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं में सुधार करेंगे।
Date: 21-06-25
विश्वसनीय कार्बन बाजार बनाने में चुनौतियां अपार
अजय त्यागी, ( लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में विशिष्ट फेलो हैं और सेबी चेयरमैन रह चुके हैं )
भारत सरकार ने जून 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) की अधिसूचना जारी की थी और उसके बाद से कई कदम उठाए गए ताकि इसको अमलीजामा पहनाया जा सके। उम्मीद है कि ट्रेडिंग 2026 में शुरू हो जाएगी और वर्ष 2027 तक इसका एक स्थिर बाजार हो जाएगा।
इस लेख में हम कार्बन बाजार बनाने के लिए सरकार के तरीकों का विश्लेषण और इसे एक सफल पहल बनाने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर बात करेंगे। इसे स्वीकारने में जरा भी संदेह नहीं है कि यह एक जटिल विषय है जिसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं। निश्चित रूप से आगे कई अतिरिक्त मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। पहले कुछ बुनियादी बातों से शुरुआत करते है। किसी भी वस्तु के बाजार के विकास के लिए वास्तविक और उचित अनुमानित मांग आवश्यक होती है। इसके बाद आपूर्तिकर्ता इसमें जुड़ते हैं और वे अपनी मांग और मूल्य का अनुमान लगाते हैं और साथ ही उस मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। यही बातें कार्बन बाजार पर भी लागू होती हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफऐंडसीसी) ने हाल ही में कुछ क्षेत्रों में चिह्नित संस्थाओं के लिए कार्बन उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य अधिसूचित किए हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो जिन संस्थाओं को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है उन्हें अपनी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता कम करनी होगी और उन लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें दंड और अन्य कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा।
स्वाभाविक रूप से, हरेक अधिसूचित संस्था को मौजूदा तकनीक, अपग्रेडेशन की आवश्यकता या ईंधन विकल्पों के संदर्भ में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आवश्यक बदलाव लाने के लिए फंडिंग की लागत का जायजा भी लेना होगा। विभिन्न संस्थाओं को अपनी उत्सर्जन तीव्रता कम करने के लिए अलग-अलग सीमांत लागतों पर विचार करना पड़ेगा। कुल उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लक्ष्य को पूरा करने के आर्थिक रूप से कुशल समाधान के लिए सुचारू तरीके से काम करने वाला कार्बन बाजार विकसित करना होगा, जहां अपेक्षाकृत अधिक सीमांत लागत वाली कंपनियां अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बाजार से कार्बन क्रेडिट खरीदने के विकल्प तलाश सकें।
आपूर्ति पक्ष में अपेक्षाकृत कम सीमांत लागत वाली कंपनियां ही होंगी जो अपने लक्ष्यों को बड़े स्तर पर हासिल कर और कार्बन क्रेडिट बेचकर पैसा कमाने का अवसर देखती हैं। इसके सफल होने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू, वास्तव में कार्बन क्रेडिट मूल्य होगा और साथ ही यह महत्त्वपूर्ण होगा कि इसका निर्धारण कितनी पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ किया जाता है। यह एक सफल कार्बन बाजार के लिए पहली बुनियादी जरूरते हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तय उत्सर्जन लक्ष्य, क्षेत्र विशेष और उस क्षेत्र की जिम्मेदार एकल इकाइयों के लिए है। लक्ष्यों को तय करने के लिए प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत, 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को 45 फीसदी तक कम करने की भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रतिबद्धता (एडीसी) रही है। एकल इकाइयों के लिए, पहले के उत्सर्जन को भी ध्यान में रखा गया है जिसमें वर्ष 2023- 24 को आधार वर्ष माना गया है।
अहम बात यह है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को शुरुआत में ही उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य तय करते हुए उन सभी उद्योगों को शामिल करना चाहिए था जिनसे सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है और इसके बाद अन्य क्षेत्रों की जिम्मेदार कंपनियों को इस दायरे में लाना चाहिए।
सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले उद्योगों में स्टील क्षेत्र को शामिल क्यों नहीं किया गया, यह बात भी समझ से परे है। इसी तरह, ताप ऊर्जा क्षेत्र जिसका कार्बन फुटप्रिंट सबसे अधिक है, उसे शायद इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि यह पहले से ही प्रदर्शन करने, लक्ष्य हासिल करने और ट्रेडिंग की योजना (पीएटी) के तहत आता है। लेकिन यह गलत धारणा है कि ऊर्जा दक्षता में सुधार से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी जरूर आएगी। इसके अलावा, एक ही लक्ष्य के लिए दो योजनाएं चलाना भी समस्या खड़ी करता है। पीएटी योजना पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझा जा सकता है कि योजना में उत्तरदायी बाध्यकारी क्षेत्रों के दायरे को सीमित करने से न केवल बाजार का आकार छोटा होगा बल्कि तरलता पर भी इसका असर पड़ेगा।
कंपनियों के लिए उनके पिछले उत्सर्जन के आधार पर लक्ष्य तय करना गलत है। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की महत्त्वाकांक्षा में कमी को दर्शाता है और इससे कार्बन क्रेडिट की पर्याप्त मांग बढ़ने की संभावना नहीं है। अहम सवाल यह भी है कि जिन कंपनियों के उत्सर्जन का पिछला रिकॉर्ड खराब रहा है, उन्हें ढील क्यों दी जाए? सही तरीका यह होगा कि एक ही क्षेत्र में एक जैसी कंपनियों को (उदाहरण के तौर पर उत्पादन क्षमता के आधार पर) वर्गीकृत किया जाए और उन सभी के लिए एक ही लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। इससे एक बेंचमार्क तैयार किया जा सकेगा और उद्योग को संसाधनों का कुशलता से उपयोग करने बेहतरतकनीक अपनाने और सही ईंधन का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा और तभी एक कार्बन बाजार तैयार हो पाएगा। सीसीटीएस ने गैर बाध्यकारी संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग में शामिल करने के लिए एक ‘ऑफसेट प्रणाली’ भी बनाई है। हालांकि, यूरोपीय संघ (ईयू) – एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स (ईटीएस) सहित दुनिया भर की उत्सर्जन ट्रेडिंग योजनाओं के अनुभव से अंदाजा होता है कि स्वैच्छिक भागीदारी से कार्बन लीकेज हो सकता है और डेटा की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है और इसके कारण योजना की साख ही खतरे में पड़ सकती है।
आप स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) के अनुभवों को ही याद करें तो यह कार्बन क्रेडिट की दोहरी गणना और खराब सत्यापन जैसी गंभीर समस्याओं से घिरी थी। योजना के शुरुआती चरण में बाजार में तरलता बनाए रखने के लिए स्वैच्छिक भागीदारी की अनुमति देने का अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाला तर्क (जिसे बाद में कम किया जाना है) सही नहीं है। यह एक कमजोर नींव पर इमारत बनाने जैसी बात है। इसके बजाय, शुरुआत सेहीबड़ी तादाद में बाध्यकारी संस्थाएं होनी चाहिए, जिन्हें मजबूत निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन तंत्र के साथ-साथ सख्त नियमों के दायरे में रखा गया हो। जानकारी के मुताबिक, ईयू ईटीएस में ऑफसेट प्रणाली पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बात करते हैं मौजूदा पीएटी योजना और सीसीटीएस के महत्त्वपूर्ण जुड़ाव के मुद्दे पर सीसीटीएस काफी हद तक पीएटी योजना पर आधारित है, जिसे 2012 से ही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) एक बाजार तंत्र के रूप में नियमों के दायरे में आने वाली संस्थाओं में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए संचालित कर रहा है। हालांकि इस तरीके के कुछ अपने निहितार्थ हैं।
सवाल यह भी है कि क्या सीसीटीएस में शामिल क्षेत्रों को कवर करने वाली पीएटी योजना समानांतर रूप से जारी रहेगी? पीएटी चक्र 8 को वर्ष 2025-26 के लिए पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है, ऐसे में यह सह-अस्तित्व कैसे काम करेगा ? बाजार को क्यों विभाजित किया जाए ? इसके बजाय सीधे उत्सर्जन तीव्रता को लक्षित करने वाली केवल सीसीटीएस ही क्यों न हो? पीएटी योजना की पहले भी आलोचना हुई है, जिसमें ढीले लक्ष्य तय करना, बाजार में ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र (ईएससीईआरटी) की अत्यधिक आपूर्ति के कारण प्रमाण पत्र की कीमतों में कमी, असंतोषजनक क्रियान्वयन और खराब तरीके का अमल शामिल है।
ऐसा लगता है कि पीएटी 3 चक्र के बाद से, विभिन्न चरणों को बंद करने के लिए आवश्यक कदम अब भी लंबित हैं। याद रहे कि पीएटी 3 चक्र, वर्ष 2017-2020 की अवधि के लिए था और इसके बाद पीएटी 4 से पीएटी 8 तक के चक्रों को अधिसूचित किया गया है। क्या इन चरणों में शामिल बाध्यकारी संस्थाओं को सीसीटीएस के तहत तभी अनुमति मिलेगी जब ये चरण बंद हो जाएंगे? पीएटी के तहत बकाया ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र को सीसीटीएस के तहत कार्बन क्रेडिट में बदलने की प्रणाली क्या होगी ? पीएटी व्यवस्था के तहत प्रचलित खराब निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन प्रक्रियाओं को देखते हुए इनकी आखिर विश्वसनीयता क्या है? क्या इन्हें सामान्य कार्बन क्रेडिट माना जाएगा या उनके लिए एक अलग वर्गीकरण या एक्सचेंज पर एक अलग ट्रेडिंग सेगमेंट होगा ? देश में एक मजबूत और विश्वसनीय कार्बन बाजार बनाने के लिए इन सभी मुद्दों पर ठीक से विमर्श और समाधान की आवश्यकता है।